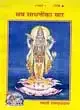|
गीता प्रेस, गोरखपुर >> ज्ञान के दीप जले ज्ञान के दीप जलेस्वामी रामसुखदास
|
108 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है ज्ञान के दीप जले...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्राक्कथन
हमारे ग्रन्थों में तथा सन्तवाणी में सत्संग और नाम-जपकी जितनी महिमा गायी
गयी है, उतनी अन्य किसी साधनकी नहीं। सत्संग के विषय में गोस्वामी
श्रीतुलसीदासजी महाराज ने यहाँ कहा है।
तात स्वर्ग अपबर्ग सुख धरिअ तुला एक अंग।
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग।।
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग।।
(मानस, सुन्दर० 4)
पुन्य पुंज बिनु मिलहिं न संता। सतसंगति संसृति कर अंता।।
(मानस, उत्तर० 45 । 3)
सतसंगत मुद मंगल मूला। सोइ फल सिधि सब साधन फूला।।
(मानस, बाल० 3 ।4)
सत्कर्म, सच्चर्चा, सच्चिन्तन और सत्संग- ये चार उत्तरोत्तर श्रेष्ठ साधन
हैं। जीवन्मुक्त तत्त्वज्ञ भगवत्प्रेमी सन्तका संग (सान्निध्य) ही वास्तव
में ‘सत्संग’ कहलाता है। इसके अतिरिक्त सच्चर्चा होती
है,
सत्संग नहीं वर्तमान में लोग प्रायः सच्चर्चा को ही सत्संग मानकर सन्तोष
कर लेते हैं। इसलिये किसी सन्तने ठीक ही कहा है कि लोग चर्चा तो सत् की
करते हैं, पर संग असत् का करते हैं; फिर कहते हैं; कि सत्संग से कोई लाभ
नहीं हुआ ! सत्संगसे लाभ न हो-यह असम्भव है।
अनुभवी सन्तकी वाणी में विशेष शक्ति होती है। अनुभवी सन्तकी वाणी गोली भरी हुई बन्दूक के समान है, जो आवाज के साथ-साथ मार भी करती है। परन्तु केवल सीखी बातें कहनेवाले वक्त की वाणी बिना गोली की बन्दूक के समान होती है जो केवल आवाज करके शान्त हो जाती है। उदाहरणार्थ-गोस्वामी श्रीतुलसीदास जी महाराज के द्वारा रामायण की रचना होने के बाद विविध कवियों ने अनेक प्रकार से रामायण की रचना की; परन्तु वे सब एक भभकेके बाद शान्त हो गयीं, जबकि गोस्वामी जी की रामायण आज भी उत्तरोत्तर विस्तार को प्राप्त हो रही है ! सन्तवाणी में आया है-
अनुभवी सन्तकी वाणी में विशेष शक्ति होती है। अनुभवी सन्तकी वाणी गोली भरी हुई बन्दूक के समान है, जो आवाज के साथ-साथ मार भी करती है। परन्तु केवल सीखी बातें कहनेवाले वक्त की वाणी बिना गोली की बन्दूक के समान होती है जो केवल आवाज करके शान्त हो जाती है। उदाहरणार्थ-गोस्वामी श्रीतुलसीदास जी महाराज के द्वारा रामायण की रचना होने के बाद विविध कवियों ने अनेक प्रकार से रामायण की रचना की; परन्तु वे सब एक भभकेके बाद शान्त हो गयीं, जबकि गोस्वामी जी की रामायण आज भी उत्तरोत्तर विस्तार को प्राप्त हो रही है ! सन्तवाणी में आया है-
वचन आगले संत का, हरिया हस्ती दंत।
ताख न टूटे भरम का, सैंधे ही बिनु संत।।
ताख न टूटे भरम का, सैंधे ही बिनु संत।।
कोई योद्धा हाथीदाँत को हाथों से पकड़कर शत्रुके किलेका द्वार खोलना चाहे
तो नहीं खोल सकेगा; क्योंकि दाँतों के पीछे हाथी (शक्ति) चाहिये ! ऐसे ही
अनुभवी सन्त वाणी हाथी दाँतों की तरह शक्ति शाली होती है, जिससे अज्ञान के
द्वार टूटे जाते हैं। ऐसे ही अनुभवी सन्तके सत्संगसे यथागृहीत बातें,
जिन्हें मैं समय-समय पर अपनी डायरी में लिखता रहा, ‘ज्ञान के
दीप
जले’ नाम से प्रकाशित की जा रही हैं। इस कार्य में पुनरुत्तियाँ
होनी स्वाभाविक हैं। परन्तु उन पुनरुक्तियों को सादक के लिये लाभप्रद
मानते हुए हटाया नहीं गया है। शुक्लयजुर्वेद- संहिता के उव्वटभाष्य में
आया है-
‘संस्कारोज्ज्वलनार्थं हितं च पथ्यं च पुनः
पुनरुपदिश्यमानं न दोषाय भवतीति’
पुनरुपदिश्यमानं न दोषाय भवतीति’
(1 । 21)
‘संस्कारोंको उद्बुद्ध करने के उदेश्य से हित तथा पथ्यकी बातका
बार-बार उपदेश करने में कोई दोष नहीं हैं।
सुनने, समझने और लिखने में पूर्ण सावधानी रखते हुए भी भूल हो सकती है। कारण कि वक्ता का जो अनुभव है, वह उसकी बुद्धि में नहीं आता। जितनी बुद्धि में आता है, उतना मनमें नहीं आता। जितना मनमें आता है उतना उसकी वाणी में नहीं आता जितना वाणी में आता है, उतना श्रोता के सुनने में नहीं आता। जितना श्रोताके सुनने में आता है, उतना उसके मन में नहीं आता। जितना मन में आता है, उतना बुद्धि में नहीं आता है, जितना बुद्धि में आता है, उतना अनुभव में नहीं आता।
सत्संग प्रेमी पाठकों से विनम्र निवेदन है कि वे इस पुस्तक में आयी बातों से लाभ प्राप्त करें और त्रुटियों को मेरी भूल समझकर क्षमा करने की कृपा करें।
सुनने, समझने और लिखने में पूर्ण सावधानी रखते हुए भी भूल हो सकती है। कारण कि वक्ता का जो अनुभव है, वह उसकी बुद्धि में नहीं आता। जितनी बुद्धि में आता है, उतना मनमें नहीं आता। जितना मनमें आता है उतना उसकी वाणी में नहीं आता जितना वाणी में आता है, उतना श्रोता के सुनने में नहीं आता। जितना श्रोताके सुनने में आता है, उतना उसके मन में नहीं आता। जितना मन में आता है, उतना बुद्धि में नहीं आता है, जितना बुद्धि में आता है, उतना अनुभव में नहीं आता।
सत्संग प्रेमी पाठकों से विनम्र निवेदन है कि वे इस पुस्तक में आयी बातों से लाभ प्राप्त करें और त्रुटियों को मेरी भूल समझकर क्षमा करने की कृपा करें।
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
विनीत
संकलनकर्ता
ज्ञान के दीप जले
पराकृतनमद्धन्धं परं ब्रह्म नराकृति। सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे
नन्दात्मजं महः।।
प्रपन्नपारिजाताय तोत्त्रवेत्रैकपाणये। ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जग्दगुरुम्।।
प्रपन्नपारिजाताय तोत्त्रवेत्रैकपाणये। ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जग्दगुरुम्।।
वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्
पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्।
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्
कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।।
हरिः ऊँ नमोऽस्तु परमात्मने नमः।
श्रीगोविन्दाय नमो नमः।
श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
महात्मभ्यो नमः।सर्वेभ्यो नमो नमः।
पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्।
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्
कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।।
हरिः ऊँ नमोऽस्तु परमात्मने नमः।
श्रीगोविन्दाय नमो नमः।
श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
महात्मभ्यो नमः।सर्वेभ्यो नमो नमः।
हमारा सम्बन्ध ईश्वर के साथ है, संसार के साथ नहीं। जिसका सम्बन्ध हमारे
साथ नहीं है, उसका त्याग करना है-
‘त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्’
(गीता 12 । 12) । जिसके साथ हमारा समेबन्ध ही नहीं, उसका त्याग क्या करें
? त्याग करना है- भूलका। सम्बन्ध भूलसे माना है। मैं शरीर हूँ और शरीर
मेरा तथा मेरे लिये है- यह सम्बन्ध माना हुआ है, वास्तव में है नहीं। शरीर
निरन्तर हमसे अलग हो रहा है। बचपन में जो शरीर था, वह अब नही है पर मैं
वही हूँ। शरीर बदल गया, पर स्वयं नहीं बदला। यह हमारा, सबका अनुभव है। इस
अनुभवका आदर करो तो जीवमुक्त हो जाओगे।
जो अपना नहीं है, उसको अपना मानने से विश्वासघात होगा, धोखा होगा ! पहले बालकपन को अपना मानते थे, वह अब रहा क्या ? शरीर निरन्तर वियोग हो रहा है।
जीव भगवान् से विमुख हुआ है, अलग नहीं और संसार के सम्मुख हुआ है, साथ नहीं। संसार से केवल सेवा के लिये ही सम्बन्ध माने। संसार को अपना और अपने लिये न माने। कोई भी काम अपने लिये न करके दूसरों की सेवा (हित)-के लिये करे। भजन-ध्यान आदि भी अपने लिये न करे।
आजकल बेटों से भी आशा मत रखो तो सुख पाओगे। उनकी सेवा करो, पर आशा मत रखो।
मैंपन हमारा स्वरूप नहीं है। ‘मैं’ (अहम्) अलग है, स्वरूप अलग है। ‘मैं’ के कारण ‘हूँ’ है। ‘मैं’ न रहे तो ‘हूँ’ नहीं रहेगा, प्रयुत ‘हैं’ रहेगा। ‘मै’ जड़ है, ‘हूँ’ चेतन है। ‘मैं हूँ’- यह चिज्जड़ग्रन्थि है। ‘मैं’ को छोड़ने सें ग्रन्थि भेद हो जाता है।परमात्मा आनन्दरूप है। संसार सुख-दुःखरूप है। दुःख के साथ जो सुख है, वह दुःख का कारण है। सुखके भोगीको दुःख भोगना ही पड़ेगा। सुखमात्र दुःखमें परिणत हो जाता है। भोगी मनुष्य सुख-दुख दोनों को भोगता है। परन्तु योगी सुख-दुःखको नहीं भोगता। यह शरीर सुख-दुःख भोगने के लिये नहीं है, प्रत्युत दोनों से ऊँचा उठकर आनन्द पाने है।
सुखदायी परिस्थिति सेवा करने के लिये है। आपमें जो बड़प्पन है, वह दूसरों का दिया हुआ है। सुखको भोगना दुःखको निमन्त्रण देना है। दुःखदायी परिस्थिति सुखकी चाहना मिटाने के लिये है।
दूसरे के दुःखसे दुःखी होनेपर हमारा दुःख मिट जाता है। दूसरे सुखी होने पर हम सुखी हो जाते हैं। काम सुख करो, आराम दूसरों को दो।
मैं –तू,यह- वह चारों एक ज्ञान के अन्तर्गत हैं। सत्ता, होनापन ज्यों-का-त्यों है। उससे यह सब प्रकाशित होता है। वह सत्ता बाहर-भीतर सब जगह परिपूर्ण है। उसमें संसार की सृष्टि-प्रलय आदि अनेक क्रियाएं होती हैं, पर उस सत्ता में, ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सत्ता ही हमारा स्वरूप है। उसी को सच्चिदानन्द कहते है। वह स्वयं प्रकाश और सबका प्रकाशक है। वह तत्त्व सब समय में सबको प्राप्त है। उस तत्त्व को जानने या न जानने से मानने या न मानने से उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस तत्त्व में कोई हलचल, आना-जाना नहीं है। जाग्रत् स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया भी उसमें नहीं है। उसी के अन्तर्गत यह सब सृष्टि है। शाखाचन्द्रन्यायसे उसका लक्ष्य कराया जाता है। उसका अनुभव करें या न करें, वह तो वैसा ही है; पर अनुभव करने से हम हलचल से (आवागमनसे) रहित हो जाते हैं। उसका अनुभव करने में मनुष्य- की जीवन की सफलता है।
जो अपना नहीं है, उसको अपना मानने से विश्वासघात होगा, धोखा होगा ! पहले बालकपन को अपना मानते थे, वह अब रहा क्या ? शरीर निरन्तर वियोग हो रहा है।
जीव भगवान् से विमुख हुआ है, अलग नहीं और संसार के सम्मुख हुआ है, साथ नहीं। संसार से केवल सेवा के लिये ही सम्बन्ध माने। संसार को अपना और अपने लिये न माने। कोई भी काम अपने लिये न करके दूसरों की सेवा (हित)-के लिये करे। भजन-ध्यान आदि भी अपने लिये न करे।
आजकल बेटों से भी आशा मत रखो तो सुख पाओगे। उनकी सेवा करो, पर आशा मत रखो।
मैंपन हमारा स्वरूप नहीं है। ‘मैं’ (अहम्) अलग है, स्वरूप अलग है। ‘मैं’ के कारण ‘हूँ’ है। ‘मैं’ न रहे तो ‘हूँ’ नहीं रहेगा, प्रयुत ‘हैं’ रहेगा। ‘मै’ जड़ है, ‘हूँ’ चेतन है। ‘मैं हूँ’- यह चिज्जड़ग्रन्थि है। ‘मैं’ को छोड़ने सें ग्रन्थि भेद हो जाता है।परमात्मा आनन्दरूप है। संसार सुख-दुःखरूप है। दुःख के साथ जो सुख है, वह दुःख का कारण है। सुखके भोगीको दुःख भोगना ही पड़ेगा। सुखमात्र दुःखमें परिणत हो जाता है। भोगी मनुष्य सुख-दुख दोनों को भोगता है। परन्तु योगी सुख-दुःखको नहीं भोगता। यह शरीर सुख-दुःख भोगने के लिये नहीं है, प्रत्युत दोनों से ऊँचा उठकर आनन्द पाने है।
सुखदायी परिस्थिति सेवा करने के लिये है। आपमें जो बड़प्पन है, वह दूसरों का दिया हुआ है। सुखको भोगना दुःखको निमन्त्रण देना है। दुःखदायी परिस्थिति सुखकी चाहना मिटाने के लिये है।
दूसरे के दुःखसे दुःखी होनेपर हमारा दुःख मिट जाता है। दूसरे सुखी होने पर हम सुखी हो जाते हैं। काम सुख करो, आराम दूसरों को दो।
मैं –तू,यह- वह चारों एक ज्ञान के अन्तर्गत हैं। सत्ता, होनापन ज्यों-का-त्यों है। उससे यह सब प्रकाशित होता है। वह सत्ता बाहर-भीतर सब जगह परिपूर्ण है। उसमें संसार की सृष्टि-प्रलय आदि अनेक क्रियाएं होती हैं, पर उस सत्ता में, ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सत्ता ही हमारा स्वरूप है। उसी को सच्चिदानन्द कहते है। वह स्वयं प्रकाश और सबका प्रकाशक है। वह तत्त्व सब समय में सबको प्राप्त है। उस तत्त्व को जानने या न जानने से मानने या न मानने से उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस तत्त्व में कोई हलचल, आना-जाना नहीं है। जाग्रत् स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया भी उसमें नहीं है। उसी के अन्तर्गत यह सब सृष्टि है। शाखाचन्द्रन्यायसे उसका लक्ष्य कराया जाता है। उसका अनुभव करें या न करें, वह तो वैसा ही है; पर अनुभव करने से हम हलचल से (आवागमनसे) रहित हो जाते हैं। उसका अनुभव करने में मनुष्य- की जीवन की सफलता है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book