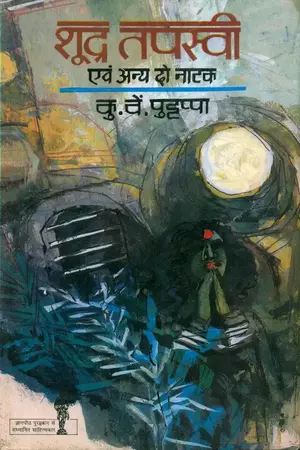|
नाटक-एकाँकी >> शूद्र तपस्वी एवं अन्य दो नाटक शूद्र तपस्वी एवं अन्य दो नाटककु. वें. पुटप्पा
|
45 पाठक हैं |
|||||||
‘शूद्र तपस्वी’ ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ साहित्य-शिल्पी कु. वें. पुटप्पा (कुवेंपु) की अद्वितीय नाट्यकृति है।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘शूद्र तपस्वी’ ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ साहित्य-शिल्पी कु. वें. पुटप्पा (कुवेंपु) की अद्वितीय नाट्यकृति है। इसमें उनके तीन नाटक-शूद्र तपस्वी, शमशान कुरुक्षेत्र और अँगूठे के बदले... सम्मिलित हैं। तीनों नाटकों का कथानक और उनके पात्र यद्यपि पौराणिक हैं, लेकिन कुवेंपु जैसे सशक्त कवि-नाटककार के तर्कपूर्ण एवं मनोवैज्ञानिक कल्पना-वैचित्र्य से तीनों रचनाएँ समकालीन जीवन-मूल्यों का साक्षात्कार कराती हैं।
कहना होगा कि तीनों नाटकों के प्रमुख नाटकों के प्रमुख पात्र निश्चित ही किसी नीति, धर्म या संकल्प को लेकर चलते हैं, फिर भी वे कहीं-न-कहीं विवश हैं उस कार्य को करने के लिए, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था।
कहना होगा कि तीनों नाटकों के प्रमुख नाटकों के प्रमुख पात्र निश्चित ही किसी नीति, धर्म या संकल्प को लेकर चलते हैं, फिर भी वे कहीं-न-कहीं विवश हैं उस कार्य को करने के लिए, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था।
कुवेंपु
राष्ट्रकवि कु.वें. पुट्टपा का काव्यनाम ‘कुवेंपु’ है। लक्ष्मी और सरस्वती के वरद-पुत्र कुवेंपु को देश ने जितना मान-सम्मान दिया है, उसका सम्पूर्ण उल्लेख करना यहाँ संभव नहीं है।
कुवेंपु का जन्म 29 दिसम्बर 1904 में कर्नाटक के शिमोगा ज़िले के पर्वतीय अंचल में स्थित तीर्थस्थल के समीप ‘कुप्पालि’ नामक एक छोटे-से ग्राम के एक सम्पन्न किसान परिवार में हुआ। उनकी आरम्भिक शिक्षा-दीक्षा गाँव में ही हुई। बाद में मैसूर के रामकृष्ण आश्रम में रहकर उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। इसके पश्चात् मैसूर विश्वविद्यालय में वे कन्नड़ प्राध्यापक के पद पर कार्य करते रहे। वहीं प्रिंसिपल बने और मैसूर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में सेवा-निवृत्त भी हुए। बहुत छोटी अवस्था में ही उन्होंने लेखनकार्य आरम्भ कर दिया था। तब उनकी विशेष रूचि कविता में ही थी। एम.ए. की कक्षा तक पहुँचते-पहुँचते वे कवि के रूप में प्रसिद्धि पा चुके थे। उनके एक अध्यापक ने एक स्थान पर लिखा है : ‘‘कवि के रूप प्रसिद्ध पुट्टपा को अपनी कक्षा में पाकर मैं दंग रह गया। ऐसा लगा मानों गोमटेश्वर की मूर्ति मानवरूप लेकर मेरे सामने आ बैठी हो।’’ कुवेंपु ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हैं। गोरा साफ़ रंग, घुँघराले बाल, चौड़ा भव्य मस्तक, सुतवाँ नाक, बड़ी-बड़ी सौम्य आँखें। साथ ही, लम्बा क़द और पुष्ट शरीर उनके व्यक्तित्व को ऐसी भव्यता प्रदान करते हैं कि कोई भी उनका सम्मान करने को विवश हो उठता है।
मूलत: कवि होकर भी कुवेंपु ने साहित्य की प्राय: सभी विधाओं पर बड़ी सफलता से लेखिनी चलायी। उनकी लेखिनी से जो कुछ भी उपजा वह सब कन्नड़ साहित्य की निधि बन गया है।
कुवेंपु में प्रसाद की दार्शनिकता, पन्त की कोमलता, निराला की ओजस्विता, और महादेवी की करुणा का अद्भुत सम्मिश्रण है। ‘सर्वोदय, समन्वय और सम्पूर्ण दृष्टि-यह मेरी कविता की त्रिवेणी है’ ये शब्द उन्होंने स्वयं अपनी कविता के बारे में कहे हैं।
उनकी कविता-सरिता अनेक-रूपों में प्रवाहित हुई है। उन्होंने गीत, खण्ड-काव्य और महाकाव्य सभी सफलतापूर्वक लिखे हैं। उनके काव्य का मुख्य स्वर राष्ट्रीयता है। कन्नड़ और कर्नाटक से अत्यधिक प्रेम होने पर भी, भारत-माँ ही उनके लिए सर्वोच्च है।
कुवेंपु गाँधी जी के स्वतन्त्रता संग्राम में पूरी तरह जुड़े रहे हैं। स्वाधीनता संग्राम और स्वाधीनता सम्प्राप्ति के लिए जन-जागरण को संबोधन के साथ-साथ उन्होंने समाज के दलित, श्रमजीवी वर्ग से अपनी कविता को जोड़ा है। कन्नड़ में ‘दलित साहित्य’ की नींव उन्होंने ही डाली है।
उनकी कालजयी कृति ‘श्रीरामायणदर्शनम्’ को 1967 में ‘ज्ञानपीठ पुरस्कार’ प्राप्त हुआ। 1955 में इसी कृति के लिए वे साहित्य अकादेमी पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं।
‘श्रीरामायणदर्शनम्’ कुवेंपु की नौ वर्ष की सफल साधना का फल है। उसकी पाण्डुलिपि देखने और उनसे मिलने के लिए एक बार श्री विनोबा भावे मैसूर पधारे थे। तब उन्होंने कुवेंपु और उनकी कृति की प्रशंसा में कहा था : ‘‘मैं यह पहले से ही जानता था कि मैसूर संस्कृति का केन्द्र है। यह प्रादेशिक कलाओं का मैका है। मैं इसे राजधानी मानकर यहाँ नहीं आया, बल्कि संस्कृति का केन्द्र मानकर यहाँ आया हूँ। इस सांस्कृतिक साम्राज्य के सम्राट हैं आप लोगों के पुट्टपा जी। वे आधुनिक वाल्मीकि हैं। इसलिए इस नगर में प्रवेश करने से पूर्व मैं उनके घर जाकर उनसे आशीर्वाद लेकर आया हूँ.....। मुझे साहसपूर्वक यह बात कहने में संकोच नहीं कि ‘श्रीरामायणदर्शनम्’ इस युग का सर्वोच्च महाकाव्य है। इसकी समानता करने वाला और कोई काव्य नहीं। यह जीवन को उच्चता की ओर ले जाता है....।’’
अत्यन्त वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और दृष्टि से उन्होंने इस महाकाव्य की रचना की है। वे दार्शनिक हैं। उनके दर्शन में एक विशिष्टता है। उन्होंने एक नव्य रामायण की रचना की है।’’
कुवेंपु के दो वृहद् उपन्यास हैं- ‘कानूरु हेग्गडिती’ और ‘मलेगलल्लि मदुमगलु’। इन दोनों का हिन्दी में अनुवाद हो चुका है।
कुवेंपु एक सफल आलोचक भी हैं। उनके आलोचनात्मक लेख साहित्य के विद्यार्थियों के लिए पथ-प्रदर्शक हैं।
इन सबके बावजूद, कुवेंपु एक महान् नाटककार हैं। कन्नड़ नाटक के इतिहास के अवलोकन से पता चलता है कि उसका श्रीगणेश अनुवाद से हुआ। आरम्भ में संस्कृत के लगभग सभी नाटकों का कन्नड़ में अनुवाद हुआ। बाद में श्री बी.एम. श्रीकण्ठैया ने कन्नड़ नाटकों की नींव रखी और उसके भविष्य की रूपरेखा निर्धारित की।
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित अन्य चार लेखकों- वेन्द्रे, कारन्त, मास्ति तथा गोकाक ने भी नाटक के क्षेत्र में कृषि की है। वैसे टी.पी. कैलासम कन्नड़ नाटक-साहित्य के पितामह हैं। ‘श्रीरंग’ का नाम कन्नड़ नाट्य-साहित्य में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने लगभग तीस नाटक और सौ एकांकी लिखे हैं। उन्होंने कन्नड़ रंगमंच को सजाया भी है और सँवारा भी। इसके अतिरिक्त कन्नड़ के क्षेत्र में पर्वतवाणी, पी. लंकेश, चन्द्रशेखर कम्बार, गिरीश कार्नाड आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।
कुवेंपु ने कन्नड़ नाटक-साहित्य में एक सुनहरा अध्याय जोड़ा है। उन्होंने तेरह नाटक लिखे हैं। ‘यमन सोलु’ (यम की हार) नाटक में उन्होंने स्वयं अभिनय भी किया। उनका ‘रक्ताक्षि’ ‘हैमलेट’ का और विरुगालि (आँधी) ‘टैम्पस्ट’ का रूपान्तर है। अन्य नाटक ‘वाल्मीकिय भाग्य’ (वाल्मीकि का भाग्य), ‘श्मशान कुरुक्षेत्र’, ‘शूद्र तपस्वी’, ‘बेरलेग कोरल’, (अँगूठे के बदले ग्रीवा), ‘चन्द्रहास’ आदि पौराणिक नाटक हैं। ‘जलगार’ (मेहतर) एक सामाजिक नाटक है। इसमें ऊँची जाति और नीची जाति के भेदभाव के खोखलेपन का उपहास किया गया है। नाटक के अन्त में स्वयं शिव एक मेहतर से कहते हैं : ‘‘तू धरती का मेहतर है, मैं सारे संसार का मेहतर हूँ।’’
प्रस्तुत संकलन में तीन नाटक हैं- ‘शुद्र तपस्वी’, ‘श्मशान कुरुक्षेत्र’, ‘अँगूठे के बदले.......’। ‘शूद्र तपस्वी’ में राम अपना दोष स्वीकार करते हैं। वे शम्बूक ऋषि का वध नहीं करते, बल्कि ब्राह्मण को अपने दोष का अनुभव कराते हैं। इस नाटक में स्वयं को ऊँची जाति का माननेवालों पर हल्का-सा व्यंग्य है।
‘श्मशान कुरुक्षेत्र’ कुवेंपु की एक और अद्भुत कृति है। युद्ध की विफलता और विनाश के साथ लेखन ने दुर्योधन की मानवता, दृढ़ता आदि सद्गुणों की ओर भी ध्यान दिलाया है। यह कन्नड़-महाभारती के अनुकूल ही है। यह नाटक धर्मवीर भारती के नाटक ‘अन्धा युग’ की भी याद दिलाता है।
‘अँगूठे के बदले.....’ (बेरलेग कोरल) नाटक में एकलव्य की मां अपने पुत्र का कटा अँगूठा देखकर द्रोण को शाप देती है- ‘‘मेरे लाल ने अपने अँगूठे की बलि जिसके लिए दी उस पापी की ग्रीवा बलि चढ़ेगी।’’ यह सुनकर एकलव्य तड़प जाता है। वह सोचता है कि उसका त्याग व्यर्थ ही गया। इससे न जाने क्या अनर्थ होगा ! इसी शाप के फलस्वरूप द्रोण की गर्दन महाभारत के युद्ध में कटकर धरती पर जा गिरती है। नाटक के महत्त्व के बारे में कुवेंपु की स्वयं लिखी टिप्पणी पठनीय है। किंवदन्ती है कि एकलव्य कर्नाटक का था। उसके चरित्र ने कितनों को ही प्रेरणा दी है। कैलासम ने भी अँग्रेजी में ‘परपज़’ नाम से एकलव्य को नायक बनाकर एक नाटक लिखा। ‘बेरलगे कोरल’ प्राचीन कन्नड़ में लिखा गया नाटक है। आधुनिक कन्नड़ में उसका वह प्रभावपूर्ण भाषा-रूप ला पाना ही संभव नहीं। बहुत प्रयास से मैंने इसका हिन्दी रूपान्तर किया है।
प्रसाद जी की भाँति कुवेंपु ने भी रंगमंच को ध्यान में रखकर नाटक नहीं लिखे, बल्कि उनकी भाषा तथा रूपकों की अभिव्यक्ति योग्य निर्देशक और रंगमंच होना चाहिए। आजकल तो रंगमंच की तकनीकि का विकास इतना हो चुका है कि कुवेंपु ने तीनों नाटकों का सफलतापूर्वक एवं प्रभावशाली मंचन हो सकता है।
आशा है, नाट्य-साहित्य में रुचि रखनेवाले सहृदय पाठकों, एवं नाटक और रंगमंच के कुशल कला-प्रेमियों को यह कृति उपयोगी सिद्ध होगी।
कुवेंपु का जन्म 29 दिसम्बर 1904 में कर्नाटक के शिमोगा ज़िले के पर्वतीय अंचल में स्थित तीर्थस्थल के समीप ‘कुप्पालि’ नामक एक छोटे-से ग्राम के एक सम्पन्न किसान परिवार में हुआ। उनकी आरम्भिक शिक्षा-दीक्षा गाँव में ही हुई। बाद में मैसूर के रामकृष्ण आश्रम में रहकर उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। इसके पश्चात् मैसूर विश्वविद्यालय में वे कन्नड़ प्राध्यापक के पद पर कार्य करते रहे। वहीं प्रिंसिपल बने और मैसूर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में सेवा-निवृत्त भी हुए। बहुत छोटी अवस्था में ही उन्होंने लेखनकार्य आरम्भ कर दिया था। तब उनकी विशेष रूचि कविता में ही थी। एम.ए. की कक्षा तक पहुँचते-पहुँचते वे कवि के रूप में प्रसिद्धि पा चुके थे। उनके एक अध्यापक ने एक स्थान पर लिखा है : ‘‘कवि के रूप प्रसिद्ध पुट्टपा को अपनी कक्षा में पाकर मैं दंग रह गया। ऐसा लगा मानों गोमटेश्वर की मूर्ति मानवरूप लेकर मेरे सामने आ बैठी हो।’’ कुवेंपु ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हैं। गोरा साफ़ रंग, घुँघराले बाल, चौड़ा भव्य मस्तक, सुतवाँ नाक, बड़ी-बड़ी सौम्य आँखें। साथ ही, लम्बा क़द और पुष्ट शरीर उनके व्यक्तित्व को ऐसी भव्यता प्रदान करते हैं कि कोई भी उनका सम्मान करने को विवश हो उठता है।
मूलत: कवि होकर भी कुवेंपु ने साहित्य की प्राय: सभी विधाओं पर बड़ी सफलता से लेखिनी चलायी। उनकी लेखिनी से जो कुछ भी उपजा वह सब कन्नड़ साहित्य की निधि बन गया है।
कुवेंपु में प्रसाद की दार्शनिकता, पन्त की कोमलता, निराला की ओजस्विता, और महादेवी की करुणा का अद्भुत सम्मिश्रण है। ‘सर्वोदय, समन्वय और सम्पूर्ण दृष्टि-यह मेरी कविता की त्रिवेणी है’ ये शब्द उन्होंने स्वयं अपनी कविता के बारे में कहे हैं।
उनकी कविता-सरिता अनेक-रूपों में प्रवाहित हुई है। उन्होंने गीत, खण्ड-काव्य और महाकाव्य सभी सफलतापूर्वक लिखे हैं। उनके काव्य का मुख्य स्वर राष्ट्रीयता है। कन्नड़ और कर्नाटक से अत्यधिक प्रेम होने पर भी, भारत-माँ ही उनके लिए सर्वोच्च है।
कुवेंपु गाँधी जी के स्वतन्त्रता संग्राम में पूरी तरह जुड़े रहे हैं। स्वाधीनता संग्राम और स्वाधीनता सम्प्राप्ति के लिए जन-जागरण को संबोधन के साथ-साथ उन्होंने समाज के दलित, श्रमजीवी वर्ग से अपनी कविता को जोड़ा है। कन्नड़ में ‘दलित साहित्य’ की नींव उन्होंने ही डाली है।
उनकी कालजयी कृति ‘श्रीरामायणदर्शनम्’ को 1967 में ‘ज्ञानपीठ पुरस्कार’ प्राप्त हुआ। 1955 में इसी कृति के लिए वे साहित्य अकादेमी पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं।
‘श्रीरामायणदर्शनम्’ कुवेंपु की नौ वर्ष की सफल साधना का फल है। उसकी पाण्डुलिपि देखने और उनसे मिलने के लिए एक बार श्री विनोबा भावे मैसूर पधारे थे। तब उन्होंने कुवेंपु और उनकी कृति की प्रशंसा में कहा था : ‘‘मैं यह पहले से ही जानता था कि मैसूर संस्कृति का केन्द्र है। यह प्रादेशिक कलाओं का मैका है। मैं इसे राजधानी मानकर यहाँ नहीं आया, बल्कि संस्कृति का केन्द्र मानकर यहाँ आया हूँ। इस सांस्कृतिक साम्राज्य के सम्राट हैं आप लोगों के पुट्टपा जी। वे आधुनिक वाल्मीकि हैं। इसलिए इस नगर में प्रवेश करने से पूर्व मैं उनके घर जाकर उनसे आशीर्वाद लेकर आया हूँ.....। मुझे साहसपूर्वक यह बात कहने में संकोच नहीं कि ‘श्रीरामायणदर्शनम्’ इस युग का सर्वोच्च महाकाव्य है। इसकी समानता करने वाला और कोई काव्य नहीं। यह जीवन को उच्चता की ओर ले जाता है....।’’
अत्यन्त वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और दृष्टि से उन्होंने इस महाकाव्य की रचना की है। वे दार्शनिक हैं। उनके दर्शन में एक विशिष्टता है। उन्होंने एक नव्य रामायण की रचना की है।’’
कुवेंपु के दो वृहद् उपन्यास हैं- ‘कानूरु हेग्गडिती’ और ‘मलेगलल्लि मदुमगलु’। इन दोनों का हिन्दी में अनुवाद हो चुका है।
कुवेंपु एक सफल आलोचक भी हैं। उनके आलोचनात्मक लेख साहित्य के विद्यार्थियों के लिए पथ-प्रदर्शक हैं।
इन सबके बावजूद, कुवेंपु एक महान् नाटककार हैं। कन्नड़ नाटक के इतिहास के अवलोकन से पता चलता है कि उसका श्रीगणेश अनुवाद से हुआ। आरम्भ में संस्कृत के लगभग सभी नाटकों का कन्नड़ में अनुवाद हुआ। बाद में श्री बी.एम. श्रीकण्ठैया ने कन्नड़ नाटकों की नींव रखी और उसके भविष्य की रूपरेखा निर्धारित की।
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित अन्य चार लेखकों- वेन्द्रे, कारन्त, मास्ति तथा गोकाक ने भी नाटक के क्षेत्र में कृषि की है। वैसे टी.पी. कैलासम कन्नड़ नाटक-साहित्य के पितामह हैं। ‘श्रीरंग’ का नाम कन्नड़ नाट्य-साहित्य में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने लगभग तीस नाटक और सौ एकांकी लिखे हैं। उन्होंने कन्नड़ रंगमंच को सजाया भी है और सँवारा भी। इसके अतिरिक्त कन्नड़ के क्षेत्र में पर्वतवाणी, पी. लंकेश, चन्द्रशेखर कम्बार, गिरीश कार्नाड आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।
कुवेंपु ने कन्नड़ नाटक-साहित्य में एक सुनहरा अध्याय जोड़ा है। उन्होंने तेरह नाटक लिखे हैं। ‘यमन सोलु’ (यम की हार) नाटक में उन्होंने स्वयं अभिनय भी किया। उनका ‘रक्ताक्षि’ ‘हैमलेट’ का और विरुगालि (आँधी) ‘टैम्पस्ट’ का रूपान्तर है। अन्य नाटक ‘वाल्मीकिय भाग्य’ (वाल्मीकि का भाग्य), ‘श्मशान कुरुक्षेत्र’, ‘शूद्र तपस्वी’, ‘बेरलेग कोरल’, (अँगूठे के बदले ग्रीवा), ‘चन्द्रहास’ आदि पौराणिक नाटक हैं। ‘जलगार’ (मेहतर) एक सामाजिक नाटक है। इसमें ऊँची जाति और नीची जाति के भेदभाव के खोखलेपन का उपहास किया गया है। नाटक के अन्त में स्वयं शिव एक मेहतर से कहते हैं : ‘‘तू धरती का मेहतर है, मैं सारे संसार का मेहतर हूँ।’’
प्रस्तुत संकलन में तीन नाटक हैं- ‘शुद्र तपस्वी’, ‘श्मशान कुरुक्षेत्र’, ‘अँगूठे के बदले.......’। ‘शूद्र तपस्वी’ में राम अपना दोष स्वीकार करते हैं। वे शम्बूक ऋषि का वध नहीं करते, बल्कि ब्राह्मण को अपने दोष का अनुभव कराते हैं। इस नाटक में स्वयं को ऊँची जाति का माननेवालों पर हल्का-सा व्यंग्य है।
‘श्मशान कुरुक्षेत्र’ कुवेंपु की एक और अद्भुत कृति है। युद्ध की विफलता और विनाश के साथ लेखन ने दुर्योधन की मानवता, दृढ़ता आदि सद्गुणों की ओर भी ध्यान दिलाया है। यह कन्नड़-महाभारती के अनुकूल ही है। यह नाटक धर्मवीर भारती के नाटक ‘अन्धा युग’ की भी याद दिलाता है।
‘अँगूठे के बदले.....’ (बेरलेग कोरल) नाटक में एकलव्य की मां अपने पुत्र का कटा अँगूठा देखकर द्रोण को शाप देती है- ‘‘मेरे लाल ने अपने अँगूठे की बलि जिसके लिए दी उस पापी की ग्रीवा बलि चढ़ेगी।’’ यह सुनकर एकलव्य तड़प जाता है। वह सोचता है कि उसका त्याग व्यर्थ ही गया। इससे न जाने क्या अनर्थ होगा ! इसी शाप के फलस्वरूप द्रोण की गर्दन महाभारत के युद्ध में कटकर धरती पर जा गिरती है। नाटक के महत्त्व के बारे में कुवेंपु की स्वयं लिखी टिप्पणी पठनीय है। किंवदन्ती है कि एकलव्य कर्नाटक का था। उसके चरित्र ने कितनों को ही प्रेरणा दी है। कैलासम ने भी अँग्रेजी में ‘परपज़’ नाम से एकलव्य को नायक बनाकर एक नाटक लिखा। ‘बेरलगे कोरल’ प्राचीन कन्नड़ में लिखा गया नाटक है। आधुनिक कन्नड़ में उसका वह प्रभावपूर्ण भाषा-रूप ला पाना ही संभव नहीं। बहुत प्रयास से मैंने इसका हिन्दी रूपान्तर किया है।
प्रसाद जी की भाँति कुवेंपु ने भी रंगमंच को ध्यान में रखकर नाटक नहीं लिखे, बल्कि उनकी भाषा तथा रूपकों की अभिव्यक्ति योग्य निर्देशक और रंगमंच होना चाहिए। आजकल तो रंगमंच की तकनीकि का विकास इतना हो चुका है कि कुवेंपु ने तीनों नाटकों का सफलतापूर्वक एवं प्रभावशाली मंचन हो सकता है।
आशा है, नाट्य-साहित्य में रुचि रखनेवाले सहृदय पाठकों, एवं नाटक और रंगमंच के कुशल कला-प्रेमियों को यह कृति उपयोगी सिद्ध होगी।
-बी.आर. नारायण
(प्रथम संस्करण से)
शूद्र तपस्वी
कथाभूमि
महान् शिल्पियों द्वारा निर्मित मन्दिर ज्यों-ज्यों पुराने होते जाते हैं। उनमें चूहे चमगादड़ आदि बिल बनाकर अपना वासस्थान बना लेते हैं। वाल्मीकि के महाकाव्य की भी यही स्थिति पैदा हो गयी है। यह तो प्राचीनता के एक अनिवार्य गुण है। लेकिन मन्दिर में पूजा करने के लिए जानेवाले लोग वहाँ के चूहों, चमगादड़ों की जिस प्रकार पूजा नहीं करते, उसी प्रकार महाकवि की कृति में प्रक्षिप्तांश के रूप में जुड़ी तथा अल्पदृष्टि के घटिया कवियों की रचनाओं को सम्मान नहीं देते। श्रीमद् रामायण में, विशेषकर उत्तरखण्ड में, ऐसे अनेक प्रक्षिप्तांश हैं। उनमें शम्बूवध भी एक ऐसा प्रसंग है। वह कहानी कुछ ऐसी है :
सीता-परित्याग के बाद एक दिन, एक वृद्ध ब्राह्मण एक मृत बालक को ले आता है। श्रीराम के प्रासाद के सामने वह बहुत विलाप करता है। अपने बेटे की अकाल मृत्यु का कारण राजा का ही कोई दोष बताता है :
सीता-परित्याग के बाद एक दिन, एक वृद्ध ब्राह्मण एक मृत बालक को ले आता है। श्रीराम के प्रासाद के सामने वह बहुत विलाप करता है। अपने बेटे की अकाल मृत्यु का कारण राजा का ही कोई दोष बताता है :
नेदृशं दृष्टपूर्वं मे श्रुतं वा घोरदर्शनम्।
मृत्युरप्राप्तकालानां रामस्य विषये यथा।।
रामस्य दृष्कृतं किंचिन्महदस्ति न संशय:।
राजद्वारि मरिष्यामि पत्न्या सार्धमनाथवत्।
ब्राह्महत्यां ततो राम समुपेत्यु सुखी भव।।
राजदोषैर्विपद्यन्ते प्रजा ह्यविधिपालिता:।
असद्वृत्ते तु नृपतावकाले म्रियते जन:।।
मृत्युरप्राप्तकालानां रामस्य विषये यथा।।
रामस्य दृष्कृतं किंचिन्महदस्ति न संशय:।
राजद्वारि मरिष्यामि पत्न्या सार्धमनाथवत्।
ब्राह्महत्यां ततो राम समुपेत्यु सुखी भव।।
राजदोषैर्विपद्यन्ते प्रजा ह्यविधिपालिता:।
असद्वृत्ते तु नृपतावकाले म्रियते जन:।।
श्रीराम मन्त्रिपरिषद् बुलाकर ब्राह्मण के लगाये अपराध के बारे में प्रश्न करते हैं। नारद एक भाषण देकर यह सिद्ध करते हैं कि शूद्र के तपस्या करने से ही ब्राह्मण की अकाल मृत्यु हुई है।
इस विषय में कुछ जानकारी यहाँ भी देखें
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book