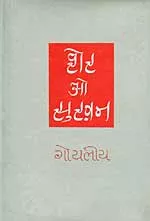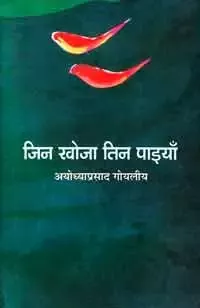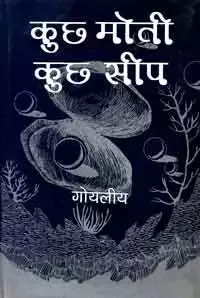|
गजलें और शायरी >> शेर-ओ-सुखन - भाग 3 शेर-ओ-सुखन - भाग 3अयोध्याप्रसाद गोयलीय
|
154 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है शेर-ओ-सुखन भाग-3....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
इन्सान की बदबख़्ती अन्दाज़ से बाहर है।
कम्बख़्त ख़ुदा होकर, बन्दा नज़र आता है।।
कम्बख़्त ख़ुदा होकर, बन्दा नज़र आता है।।
आज़ाद अन्सारी
बरहमन नाम-ए-नाक़ूस मस्जिद तक भी पहुँचा दे।
बुरा क्या है मुअज़्ज़न भी अगर बेदार हो जाये।।
बुरा क्या है मुअज़्ज़न भी अगर बेदार हो जाये।।
हफ़ीज़ जालन्धरी
‘शाद’ अज़ीमाबादी
ख़ान बहादुर नवाब सैयद अलीमुहम्मद ‘शाद’ 1846 ई. में
उत्पन्न
हुए और 1927 ईं में समाधि पाई। नियाज़ फ़तेहपुरी के शब्दों
में-‘‘शाद ब-लिहाज़ तग़ज़्ज़ुल बड़े मर्तबे के शायर
थे। उनके
यहां मीर-ओ दर्दका गुदाज़, मोमिन की नुक्तासंजी, ग़ालिबकी बुलन्द परवाज़ी
और अमीर-ओ-दाग़की सलासत सब एक ही वक़्तमें ऐसी मिली-जुली नज़र आती है कि
अब ज़माना मुश्किलसे ही कोई दूसरी नज़ीर पेश कर
सकेगा।’’1
‘शाद’ अज़ीमाबाद (पटना सिटी) के रहनेवाले थे। वे ख़्वाजा मीर ‘दर्द’ की शिष्य परम्परामें हुए हैं। अतः आपके कलाम में भी वह असर नज़र आता है। कहीं-कहीं तत्कालीन लखनवी रंग की भी झलक मारती है। आप मीर ‘अनीस’ से भी काफ़ी प्रभावित नज़र आते हैं।
शाद देहलवी-लखनऊ ज़बान के क़ायल नहीं थे। यही कारण है कि उनके कलाम में यत्र-तत्र मुहावरों और शब्दों का प्रयोग उक्त स्थानों की परम्परासे भिन्न हुआ है।
‘शाद’ ख़्वाजा ‘दर्द’ स्कूलके स्नातक थे। इसलिए हमने आपको
———————————————
‘इन्तक़ादियात, भाग 2, पृ. 156।
मजलिसे-देहलीमें उच्चासन दिया है। आपका कलाम भी ईश्वरीय-प्रेम अध्यात्मिकता और दार्शनिकतासे ओत-प्रोत है। आपका रंगे शायरी ख़्वाजा ‘आतिश’1 से बहुत कुछ समानता रखता है।
‘आतिश’ और ‘शाद’ दोनों ही अपने-अपने युग में बहुत बुलन्द मर्तबेके शायर हुए हैं। दोनोंके विचार, भाव और अन्दाज़े-बयान मिलते-जुलते हैं। दोनोंकी अक्सर ग़जलें हमतरही ऐसी हैं कि अगर उनमेंसे उपनाम निकाल दिया जायें तो कौन ग़ज़ल किसकी है, निश्चयपूर्वक कहना आसान नहीं। ज़ाहिरामें दोनों लखनवी, किन्तु भावों और विचारकोंकी दृष्टिसे अंतरंगमें देहलवी हैं। दोनों ही सूफ़ियाना विचारके हैं।
इतनी समानता होते हुए भी दोनों का रंग भिन्न-भिन्न है। ‘आतिश’ के यहाँ व्यंग्य और तीखापन इस ग़ज़बका है कि कुछ न पूछिये। उनके काल में गर्मी, और अन्दाज़ेबयान में तड़प इस बला की है कि कोई भी शायर उनका हमसर नज़र नहीं आता। ‘आतिश’ के यहाँ दुःख-दर्द, पीड़ा-व्यथामें भी मुस्कान भरी है। उनके ग़म में भी एक लहक और चहक होती है।
‘शाद’ अज़ीमाबाद (पटना सिटी) के रहनेवाले थे। वे ख़्वाजा मीर ‘दर्द’ की शिष्य परम्परामें हुए हैं। अतः आपके कलाम में भी वह असर नज़र आता है। कहीं-कहीं तत्कालीन लखनवी रंग की भी झलक मारती है। आप मीर ‘अनीस’ से भी काफ़ी प्रभावित नज़र आते हैं।
शाद देहलवी-लखनऊ ज़बान के क़ायल नहीं थे। यही कारण है कि उनके कलाम में यत्र-तत्र मुहावरों और शब्दों का प्रयोग उक्त स्थानों की परम्परासे भिन्न हुआ है।
‘शाद’ ख़्वाजा ‘दर्द’ स्कूलके स्नातक थे। इसलिए हमने आपको
———————————————
‘इन्तक़ादियात, भाग 2, पृ. 156।
मजलिसे-देहलीमें उच्चासन दिया है। आपका कलाम भी ईश्वरीय-प्रेम अध्यात्मिकता और दार्शनिकतासे ओत-प्रोत है। आपका रंगे शायरी ख़्वाजा ‘आतिश’1 से बहुत कुछ समानता रखता है।
‘आतिश’ और ‘शाद’ दोनों ही अपने-अपने युग में बहुत बुलन्द मर्तबेके शायर हुए हैं। दोनोंके विचार, भाव और अन्दाज़े-बयान मिलते-जुलते हैं। दोनोंकी अक्सर ग़जलें हमतरही ऐसी हैं कि अगर उनमेंसे उपनाम निकाल दिया जायें तो कौन ग़ज़ल किसकी है, निश्चयपूर्वक कहना आसान नहीं। ज़ाहिरामें दोनों लखनवी, किन्तु भावों और विचारकोंकी दृष्टिसे अंतरंगमें देहलवी हैं। दोनों ही सूफ़ियाना विचारके हैं।
इतनी समानता होते हुए भी दोनों का रंग भिन्न-भिन्न है। ‘आतिश’ के यहाँ व्यंग्य और तीखापन इस ग़ज़बका है कि कुछ न पूछिये। उनके काल में गर्मी, और अन्दाज़ेबयान में तड़प इस बला की है कि कोई भी शायर उनका हमसर नज़र नहीं आता। ‘आतिश’ के यहाँ दुःख-दर्द, पीड़ा-व्यथामें भी मुस्कान भरी है। उनके ग़म में भी एक लहक और चहक होती है।
क़फ़समें भी है वही चहचहा गुलिस्तांका
शाद के यहाँ रंजो-ग़म, दर्दो-अलम, व्यथापूर्ण हैं।
‘आतिश’ इस
विषय में ‘ग़ालिब’ के अधिक समीप हैं और
‘शाद’
‘मीर’ के नज़दीक हैं। ‘आतिश’
रंजो-ग़ममें बिलखते
नहीं, यहाँ तक कि वे हृदयकी पीड़ा को व्यक्त करना भी अपनी शान के ख़िलाफ़
समझते हैं—
जौरो-ज़फ़ायेयारसे2 रंजो-महन3 न हो।
दिलपर हूजेमेग़म हो, जबींपर शिकन न हो।।
दिलपर हूजेमेग़म हो, जबींपर शिकन न हो।।
——————————————
1.‘आतिश’ का परिचय एवं कलाम ‘शेरो सुख़न’ प्रथम भाग में दिया जा चुका है। 2.प्रेयसीके अत्याचार करने पर; 3.दुखी और व्यथित न हो।
‘शाद’ व्यथा पीड़ाके आँसुओंको पीनेके बजाय उन्हें, प्रकट करना आवश्यक समझते हैं—
1.‘आतिश’ का परिचय एवं कलाम ‘शेरो सुख़न’ प्रथम भाग में दिया जा चुका है। 2.प्रेयसीके अत्याचार करने पर; 3.दुखी और व्यथित न हो।
‘शाद’ व्यथा पीड़ाके आँसुओंको पीनेके बजाय उन्हें, प्रकट करना आवश्यक समझते हैं—
ख़ामोशीसे मुसीबत और भी संगीन होती है।
तड़प ऐ दिल तड़पनेसे ज़रा तकसीन होती है।।
यूँ ही रातों को तड़पेंगे, यूँ ही जाँ अपनी खोयेंगे।
तेरी मर्ज़ी नहीं ऐ दर्देदिल ! अच्छा ! न सोयेंगे।।
तड़प ऐ दिल तड़पनेसे ज़रा तकसीन होती है।।
यूँ ही रातों को तड़पेंगे, यूँ ही जाँ अपनी खोयेंगे।
तेरी मर्ज़ी नहीं ऐ दर्देदिल ! अच्छा ! न सोयेंगे।।
मगर वे अन्य शायरोंकी तरह सरे आम हाय-हाय करनेके पक्षपाती नहीं—
तड़पना है तो जाओ जाके तड़पो ‘शाद’ ख़िलवतमें।
बहुत दिनपर हम इतनी बात गुस्ताख़ाना कहते हैं।।
बहुत दिनपर हम इतनी बात गुस्ताख़ाना कहते हैं।।
इन दोनों के कलाममें उल्लेखनीय विशेष अन्तर यह है कि
‘आतिश’
के यहाँ पतित भाव, हक़ीर विचार और बाज़ारी इश्क़ अधिकांश रूपमें पाया जाता
है। लेकिन ‘शाद’ के कलाममें इतनी संजीदगी, बड़प्पन,
और सुथरा
पन पाया जाता है कि वे उर्दू-शायरों में सर्वश्रेष्ठ नज़र आते हैं।
उर्दूके सर्वश्रेष्ठ शायर ‘मीर’ भी अपना दामन इब्तज़ाल (कमीने ज़लील विचारों) से न बचाये रख सके। बक़ौल किसीके ‘‘उनके दीवान में लौंडे भरे पड़े हैं’’ ‘ग़ालिब’ भी धौल-धप्पेपर उतारू हो जाते हैं—
उर्दूके सर्वश्रेष्ठ शायर ‘मीर’ भी अपना दामन इब्तज़ाल (कमीने ज़लील विचारों) से न बचाये रख सके। बक़ौल किसीके ‘‘उनके दीवान में लौंडे भरे पड़े हैं’’ ‘ग़ालिब’ भी धौल-धप्पेपर उतारू हो जाते हैं—
धौल-धप्पा उस सरापा नाज़का शेवा नहीं।
हम ही कर बैठे थे ‘ग़ालिब’ पेश दस्ती एक दिन।।
हम ही कर बैठे थे ‘ग़ालिब’ पेश दस्ती एक दिन।।
और ‘मोमिन’ का तो माशूक़ ही हरजाई नहीं, स्वयं भी
हरजाई थे। हमेशा मृगनयनियों (ग़ज़ालचश्मों) को फाँसते रहे—
आये ग़ज़ालचश्म सदा मेरे दाममें।
सैयद ही रहा मैं, ग़िरफ़्तार कम हुआ।।
सैयद ही रहा मैं, ग़िरफ़्तार कम हुआ।।
तात्पर्य यह है कि प्राचीन और अर्वाचीन प्रायः सभी शायरों के कलाममें यह
दोष पाये जाते हैं। लेकिन ‘शाद’ का कलाम उन दोषोंसे
मुक्त है।
उनके यहाँ ‘बोसा’ (चुम्बन) जैसा बदनाम और हक़ीर शब्द
भी इतनी
बुलन्दी से नज़्म हुआ है कि अन्यत्र मिसाल नहीं मिलती।
बोसये-संगे-आस्ताँ1 हिल न सका हज़ार हैफ़।
आगे क़दम न बढ़ सका हिम्मते-सरफ़राज़का2।।
आगे क़दम न बढ़ सका हिम्मते-सरफ़राज़का2।।
उक्त शेर की पवित्रता और मर्तबे को वही अनुभव कर सकता है, जिसने कभी
संगे-आस्ताँ के बोसा लेने का प्रयत्न किया हो, परन्तु किसी कारण सफलता न
मिली हो। राष्ट्रपिता बापूके शहीद किये जानेपर उनकी चिताकी राख लेने के
लिए लाखों नर-नारी लालायित थे। एक-दूसरे को धकेलकर बापूकी राखको मस्तकसे
लगानेको कई लाख नर-नारी बढ़ रहे थे, परन्तु कितनोंको सफलता मिली ? जो भी
राख न पा सके, अपने भाग्य को कोस रहे थे। जब किसी की ऐसी स्थिति हो, तभी
‘साद’ के उक्त शेरकी महत्ता प्रकट हो सकती है।
आस्ताने-यार या
शहीदों-की समाधियोंको बोसा देना ‘साद’ की अछूती और
उच्च भावना
है—
शहीदाने-वफ़ाकी ख़ाक, क्या अक्सीरसे कम है ?
न हाथ आये क़दम, बोसा तो ले जाकर मज़ारोंका।।
न हाथ आये क़दम, बोसा तो ले जाकर मज़ारोंका।।
यह बात ‘ग़लिब’ और ‘आतिश’ को
कहाँ नसीब ?
‘ग़ालिब’ तो स्वयं ही अपने इस हक़ीर ख्यालसे भयभीत
नज़र आते
हैं—
——————————
1 माशूक़की चौखट के पत्थरका चुम्बन; 2 अभिमानके साहसका।
——————————
1 माशूक़की चौखट के पत्थरका चुम्बन; 2 अभिमानके साहसका।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book