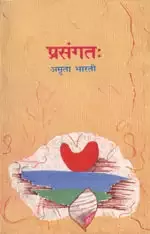|
लेख-निबंध >> प्रसंगतः प्रसंगतःअमृता भारती
|
110 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है प्रसंगतः...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘प्रसंगतः’ में संग्रहीत सामग्री के विषय ऐसे तो हैं ही जिनसे
अमृता भारती वर्षों से निरन्तर उलझती रही हैं। साथ ही ऐसे विषय-संदर्भ भी
हैं जिनकी चुनौतियों से किसी भी सजग और समर्थ समकालीन लेखक के लिए कतराना
असम्भव है। इसमें साहित्य की विभिन्न विधाओ—निबन्ध, पत्र,
व्यक्तिचित्र, एकालाप डायरी आदि के माध्यम से लेखक और लेखन की प्रकृति,
परिवेश और उसकी स्थिति तथा सम्बन्धों का परिष्कृत और विलक्षण
विवेचन-सम्प्रेषण है। इस दृष्टि से कह सकते हैं कि ‘प्रसंगतः’
का गद्य ऐसे निखार और शिखर पर है जो निस्सन्देह दुर्लभ है।
इस पुस्तक में वह सब-कुछ मौजूद है जो सर्जना के स्तर पर समय तथा साहित्य के कई आयामों को बड़ी गम्भीरता, लेकिन सहजता के साथ उजागर करता है; और पाठक को संवाद के लिए आमन्त्रित भी करता है। दूसरे शब्दों में, एक निश्चित काल और इतिहास में ‘प्रसंगतः’ मनुष्य, समाज और उनकी नियति की खोज की सार्थक प्रक्रिया और आत्मीय स्वीकार है। उन तमाम प्रश्नों को समझने और उनके उत्तर पाने की प्रसंगतः कोशिश है जो सामयिक और शाश्वत दोनों हैं।
इस पुस्तक में वह सब-कुछ मौजूद है जो सर्जना के स्तर पर समय तथा साहित्य के कई आयामों को बड़ी गम्भीरता, लेकिन सहजता के साथ उजागर करता है; और पाठक को संवाद के लिए आमन्त्रित भी करता है। दूसरे शब्दों में, एक निश्चित काल और इतिहास में ‘प्रसंगतः’ मनुष्य, समाज और उनकी नियति की खोज की सार्थक प्रक्रिया और आत्मीय स्वीकार है। उन तमाम प्रश्नों को समझने और उनके उत्तर पाने की प्रसंगतः कोशिश है जो सामयिक और शाश्वत दोनों हैं।
पूर्व शब्द
जीवन का रफ्तार इस अर्थ में काफी तेज रही कि कभी रुकना न
हुआ—पड़ावों पर, वस्तुओं और व्यक्तियों के अन्दर। जैसे, सब हाथ
से
सरकता चला गया या झर गया। आज जिस निष्कर्ष के अन्दर हूँ—वह भीतर
की
असम्पृक्त रहने वाली एक स्त्री का परिमण्डल है। परम प्रेममयी और सुन्दर
स्त्री का परिमण्डल। स्वभाव का आसक्तियोग अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ,
पर फिर भी,—सम्बन्धों के आग्रह और जुड़ाव अब सिर की चादर नहीं
बनते,
जैसे सब कुछ अंगुल की दूरी से गुजरता है—आघात या आमन्त्रण।...
पिछले 20-25 वर्षों के चलते-जाते (क्योंकि बैठना नहीं हुआ था) जो कुछ भी लिखा गया और जो फाड़ा नहीं गया, उसमें से काफी कुछ बिना किसी संशोधन-परिमार्जन के इस संकलन के अन्दर है। किताब का शीर्षक ‘प्रसंगतः’ रचनाओं की विभिन्नता से जुड़ा है। समय, स्थान, घटना-क्रम, पात्र और विधाएँ सभी अलग हैं—और वे किसी न किसी प्रसंग के दायरे में हैं। ‘अपने तहत’ के कुछ पृष्ठ अवश्य इस दायरे की सीमा लाँघ गये हैं, शायद यही उनकी चरितार्थता भी है। और इस पुस्तक का अन्तिम पृष्ठ अपने शीर्षक की तरह ही मेरे जीवन का भी संक्षिप्त ‘सारांश’ है—अपनी व्यापकता के कारण।
खर्च हुई इतनी सारी स्याही के अन्दर अगर कहीं कोई रोशनी की लकीर खिंच सकी है, तो उसे मैं कृतज्ञता की तरह स्वीकार करती हूँ।....
पिछले 20-25 वर्षों के चलते-जाते (क्योंकि बैठना नहीं हुआ था) जो कुछ भी लिखा गया और जो फाड़ा नहीं गया, उसमें से काफी कुछ बिना किसी संशोधन-परिमार्जन के इस संकलन के अन्दर है। किताब का शीर्षक ‘प्रसंगतः’ रचनाओं की विभिन्नता से जुड़ा है। समय, स्थान, घटना-क्रम, पात्र और विधाएँ सभी अलग हैं—और वे किसी न किसी प्रसंग के दायरे में हैं। ‘अपने तहत’ के कुछ पृष्ठ अवश्य इस दायरे की सीमा लाँघ गये हैं, शायद यही उनकी चरितार्थता भी है। और इस पुस्तक का अन्तिम पृष्ठ अपने शीर्षक की तरह ही मेरे जीवन का भी संक्षिप्त ‘सारांश’ है—अपनी व्यापकता के कारण।
खर्च हुई इतनी सारी स्याही के अन्दर अगर कहीं कोई रोशनी की लकीर खिंच सकी है, तो उसे मैं कृतज्ञता की तरह स्वीकार करती हूँ।....
अमृता
प्रसंगतः
साप्ताहिक ‘नवजीवन पथ’ के सम्पादन-काल के दौरान
सामयिक
प्रतिक्रिया के रूप में नवम्बर 1973 से जनवरी 1974 के बीच प्रकाशित कुछ
वक्त्व्य...
पर, लिखा गया हर शब्द सिर्फ सामयिक नहीं होता, वह समय की चेतना को स्पर्श करता हुआ उससे आगे भी जाता है।
शायद इन पृष्ठों में ऐसा हुआ हो।
जीवन और जगत् की दिशा में जब भी हमने सोचने की कोशिश की, हमेशा एक टकराहट का सामना करना पड़ा। दरअसल प्रश्न इतने ज्यादा हैं और समाधान इतने कम की चीजें विरोधी रूप धारण करके अपने हल की दिशा में बढ़ने के बजाए आपस में ही टकराने लगती हैं। इस टकराहट को संघर्ष कहना, और वह भी सृजनशील संघर्ष कहना, जरा भी मुनासिब नहीं होगा। संघर्ष एक जागरुक प्रयत्न है जिसका उद्देश्य निश्चित और स्पष्ट है होता है। धर्म के नाम पर हो या आध्यात्मिकता के नाम पर, परम्परा के नाम पर हो या आधुनिकता के नाम पर, प्रगतिशीलता हो या प्रतिक्रियाशीलता, कोई भी अन्धा प्रयत्न संघर्ष नहीं कर सकता, और इसलिए वह कभी भी क्रान्ति में, एक सफल और निश्चित परिणामवाली क्रान्ति में नहीं ढल सकता।
आज रास्ता चलते हम हवाओं में गर्मी महसूस करते हैं। तापमान हर रोज बढ़ रहा है और साथ ही भारीपन भी। यह हवाओं में छुपी हुई उस आग का सूचक है, जो किसी भी क्षण विस्फोट का रुप ले सकती है। हम सब इस सम्भावित विस्फोट के नीचे खड़े हैं। हमारे अपने ही नष्ट हो जाने का खतरा है। अगर हम इस आग को वैदिक ऋषि के सदृश्य सृष्टि की ऋचा की तरह नहीं रच सके, तो हमें उस नुकसान को सहन करना पड़ेगा जो देखने में लपट को ऊँची करने का प्रयत्न लगता है, लेकिन जो सिर्फ धुआँ होकर रह जाता है। हमें इस आग को अपने अग्रणी क्रान्ति-पुरुष का मस्तक बनाना है। इसे वह स्वरूप देना है, जिसमें हम अपनी वास्तविक दुनिया का दर्शन कर सकेंगे। हमें इस अग्नि की उज्ज्वलता में से वह मेधा बटोरनी है, जिससे युक्त होकर हम अपने झितिजों को अन्धकारमुक्त कर सकेंगे। यह सही है कि आग है और वह हवाओं की मर्जी पर किसी भी दिशा में तेजी पकड़ सकती है, पर आग को हिलाने से पहले क्या यह जरूरी नहीं है कि हम हवाओं को वह रुख दें, जो हमारा अपना रुख हो, हमारी अपनी दिशा। जब तक हिन्दुस्तान की आँखें अपनी नासिका के अग्रभाग पर केन्दित नहीं होंगी तब तक वह पराये प्रभावों के कुचक्र में फँसा रहेगा। गीता का अपने से अपने को देखना ‘आत्मनात्मानं पश्येत्’ और बुद्ध का ‘अप्पदीपो भव’ उपदेश इसी ज्ञान का निर्णय करते हैं। इस सन्दर्भ में यह दोहराना जरूरी है कि हमें अपना लक्ष्यभेद अपने ही तीर से करना होगा।
अगर हमें क्रांति के बीजों को हिन्दुस्तान की धरती पर बोना है तो पहले इस धरती के चरित्र को पहचान लेना होगा। इस भूमि ने उन बीजों को भी कभी अंकुरित नहीं किया जो इसके निजी व्यक्तित्व या स्वधर्म के विरुद्ध पड़ते हैं। अपनी स्वाभाविक करुणा से इसने उनका विनाश भले ही किया हो, पर ज्यों का त्यों वमन जरूर कर दिया। इस वमन के पीछे उन कारणों को तलाशना व्यर्थ होगा, जो धरती को अनुर्वरा घोषित करते हैं और उस खाद को भी डालना व्यर्थ होगा, जो भूमि के निजी गुण का हनन कर इन बीजों को प्रतिफलित करने में मदद करती है। हमें वह फसल उगानी होगी जो हमेशा ही हमें पुष्ट और सबल बनाती रही है। इस दृष्टि से हमें सिर्फ सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक क्रान्ति से ही नहीं गुजरना, बल्कि धर्म, दर्शन, संस्कृति, कला और अध्यात्म की दिशा में भी रूपान्तरण प्रस्तुत करना है। उन सब मूल्यों को साथ लेकर चलना है, जिनसे भारतीय मानस अभिच्छेद्य रूप से जुड़ा है। एक तरफ हमें अनास्था, सतही बौद्धिकता, अकर्मण्य प्रगतिशीलता और निष्प्रेम विद्रोह के बुलबुलों को फोड़ना है तो दूसरी तरफ अन्धविश्वास, आडम्बर और तथाकथित गुरुओं की बढ़ती हुई भीड़ में से जागरुक विश्वास, सत्यनिष्ठा और उस ‘नेतृत्व’ को तलाशना है, जो न केवल हमारे जागतिक व्यक्तित्व और स्वातन्त्र्य के लिए, बल्कि हमारी आत्मा के लिए भी प्रसिद्ध हो।
जब हम आत्मिक प्रतिबद्धता की बात करते हैं, तब अन्य कोई भी पक्ष अप्रतिश्रुति नहीं रह जाता। वास्तव में सम्पूर्ण दायित्व और सम्पूर्ण स्वीकार अथवा सम्पूर्णता मात्र ही आध्यात्मिक जीवन का यात्रा-प्रसंग है।
विश्व के सभी धर्मग्रन्थों में यह प्रतिबद्धता निश्चित भाषा में प्रकट हुई है। श्रीकृष्ण की अर्जुन के प्रति की गयी यह प्रतिज्ञा—‘मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे’ मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मुझे ही प्राप्त होगा, तू मुझे प्रिय है—आगे और भी स्पष्ट हो जाती है, जब वे कहते हैं ‘अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः’— मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूँगा, तू चिन्ता मत कर। ये शब्द किसी भी पूर्वापरता से स्वतन्त्र अपने परिणाम में स्वयं समर्थ हैं, क्योंकि भगवदीय वचनों की सार्थकता किसी भी ‘पर’ पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। लेकिन इस तथ्य की विषद व्याख्या हमारा प्रस्तुत प्रसंग न होने के कारण हम उन वाक्यों के बारे में सोचते हैं, जो इस प्रतिश्रुति में शर्त की तरह ध्वनित होते हैं।
‘मुझमें अपना मन लगा’ मेरा भक्त बन, मुझे नमन कर, एक मात्र मेरी शरण में आ’ मानो ये सब अपेक्षायें पूरी किये बगैर वह प्रतिज्ञा एक कमजोर आश्वासन मात्र रह जाती है। इसी तरह ‘परशुराम-कल्पशूत्र’ का यह शूत्र ‘अनुग्रहः
संश्रितेषु—आश्रितों को भगवदीय कृपा प्राप्त होती है—एक शर्त है, क्योंकि कृपा मुक्त नहीं है, ‘आश्रय-भाव’ में बद्ध है। बुद्ध ने भी बार-बार कहा है ‘बुद्ध की शरण में आ, धर्म की शरण में, संघ की शरण आ, दुःखों का निवारण तभी हो सकेगा। ‘ईसा ने कहा’, ‘जो मेरे पास आयेगा, उसके सब पाप क्षमा कर दिये जायेंगे, जो मेरा विश्वास करेगा, वह स्वर्ग के साम्राज्य में प्रवेश पायेगा।’ इन सब भगवद पुरुषों के ये कथन उस प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं, जो अपने निजी नियमों में चलती है या अपने प्रतिफल के लिए दूसरे पक्ष में एक विशिष्ट स्थिति की या मनोवृत्ति की माँग करती है। इसलिए प्रतिबद्धता सिर्फ शरणागत के लिए होने के कारण व्यक्तिपरक होकर रह जाती है। यह व्यक्ति के लिए ऐकान्तिक कल्याण का प्रतीक है, समाज से जिसका कोई प्रकट और समर्थ सम्बन्ध नहीं है।
तो क्या हम यह विश्वास करें कि भगवदीय प्रेम और व्यक्ति की निष्कृति इस सापेक्ष सम्बन्ध में निहित है ?
वस्तुतः यह प्रतिज्ञा व्यक्ति और भगवान् के बीच के निजी सम्बन्ध की सूचक है, जो सम्बन्ध काफी लम्बी आत्मिक यात्रा के बाद सिद्ध होता है। अब हम उस प्रतिज्ञा की बात करेंगे, गीता ने जिसे अत्यन्त व्यापक या वैश्विक सन्दर्भ में प्रकट किया है, और ‘अवतारवाद’ सिद्धान्त के विचार-विमर्श में जिसका मामूली अनपढ़ व्यक्ति और प्रकाण्ड पण्डित एक साथ करता है ‘यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ! अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।’—इस सन्दर्भ में हम किसी अवतरण की व्याख्या न कर, उस प्रतिबद्ध पुरुष के जन्म की बात करेंगे, जो सचमुच ही अपने इस वचन को निभाने में समर्थ है। ‘धर्म की ग्लानि’ मानव-जीवन के उन आन्तरिक मूल्यों का पतन, है जो उसे मनुष्य होने के सौन्दर्य-गुण से मण्डित करते हैं। कोई भी विघटन धर्म की इस सुद़ढ़ आधारशिला की टूटन ही है। जीवन के वे मूल्य, जो ‘अस्ति’ भाव के प्रतीक हैं, जब धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक साहित्यक और सांस्कृतिक क्षेत्र में तथा सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत सम्बन्धों की दिशा में अपना वजन खो बैठते हैं, वहीं से ‘धर्म की ग्लानि’ शुरू हो जाती है। उस ‘अस्ति’ भाव की प्रतिष्ठा इस प्रतिज्ञात पुरुष के जन्म के कारण बनती है। पहली प्रतिज्ञा की तरह यह दूसरी प्रतिज्ञा सृष्टि के प्रथम दिनारम्भ से अब तक अपने तदर्थ में ज्यों की त्यों बनी हुई है।
इसी प्रतिज्ञा का दूसरा भाग है, ‘परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्’— साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए मैं अपने को रचता हूँ। साधुजन सिर्फ ईश्वरवादी लोग ही नहीं, वे निरीह सज्जन प्राणी भी हैं, जो अपने छोटे-छोटे सत्यों को अब भी अपने हृदय से लगाये निरन्तर संघर्षरत हैं। किसी बड़े दार्शनिक या वैचारिक या बौधिक सत्य का चेहरा इन्होंने भले ही न देखा हो, लेकिन जो अपनी नन्हीं आस्थाओं के बल पर अब भी हर सुबह उगते हुए सूर्य को ‘मित्र’ कहकर सम्बोधित करते हैं। इन निरीह कोमल प्राणियों की रक्षा ईश्वर का निजी कृत्य है या कहें दायित्व है, जिसके लिए सीधी सरल ‘साधुता’ के अतिरिक्त अन्य कोई अपेक्षा नहीं है।
लेकिन उपर्युक्त वाक्य के उत्तरार्ध में एक तीसरी प्रतिज्ञा या प्रतिबद्धता है दुर्जनों के लिए। ‘निरवैरः सर्वेभूतेषु यः स मामेति पाण्डव’—जो सब प्राणियों में वैररहित है, वह मुझे प्राप्त करता है यह जिसकी प्राप्ति की शर्त है, वह स्वयं ‘दुर्जन’ के प्रति कैसे वैर रख सकता है ? उसका उनके प्रति भी उसी तत्परता से प्रतिबद्ध होना उसके अपने चरित्र की अनिवार्यता है। जो दुष्ट हैं, पापी है, दरिद्र हैं, मलिन हैं, अन्यायी और अत्याचारी हैं, निष्प्रेम और निष्करुण हैं, वे उसके अपने शरीर का व्रण हैं।
वह इस ‘व्रण’ का उपचार कई तरह से करता है, कभी औषधि कभी प्रलेप द्वारा, कभी शल्य द्वारा। जब वह दुर्जनों के विनाश की बात करता है, तब साधुओं के परित्राण की सापेक्षता के कारण नहीं, स्वयं दुर्जनों को उनकी ‘कर्दम-कृमिता’ से उबार लेने के लिए, जिसमें वे संस्कारगत रूप में पड़े हुए हैं। दुर्जनों का यह विनाश या हिंसा द्वेषप्रेरित नहीं है, ठीक उसी प्रेम और करुणा का आयोजन है, जिससे वह साधुओं के परित्राण के लिए प्रेरित होता है। महाभारत युद्ध की रंग-रचना करनेवाले श्रीकृष्ण किसी व्यक्ति, जाति, समाज अथवा पक्ष के हित या अहित में इस युद्ध के सूत्रधार नहीं हैं, बल्कि पृथ्वी पर अपने होने की प्रतिज्ञा के पीछे जो कारण है, उसकी सिद्धि के लिए ही इस रक्त-अनुष्ठान की रचना करते हैं।
तो क्या हम धर्म के प्रति, साधु के प्रति, दुर्जन के प्रति, विश्व की चतुर्मूर्ति के प्रति प्रतिबद्ध इस पुरुष की प्रतीक्षा करें या राष्ट्र के हृदय की दबी हुई आग में इस ‘हृत्पुरुष’ का जन्म हो चुका है ?
समाज और व्यक्ति-व्यक्ति के बीच की विषमताओं और विभेदताओं के हल करने के लिए यह जरूरी है कि शासन इस विभेद को मिटाये और एक समान व्यवस्था को कायम करे। इस विषमता और विभेद की रचना करने वालों की संख्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इन ‘व्यक्ति विशेषों’ के साथ आम आदमी की बहुत बड़ी संख्या भी जुड़ी हुई है, जो इस खाई को गहरा और चौड़ा करने के लिए अपने हाथ में कुदाली, फावड़ा लिए खड़ी है। यह आम आदमी अपने दैनिक सत्य (रोटी) के लिए महत्तर सत्य के प्रति विमुख रहने के लिए विवश है, जो यह कहता है ‘मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है।’
खाई के वे रबर-सिरे किसी भी क्षण उन लोगों से छीने जा सकते हैं जो इसे लगातार खींचते जा रहे हैं और ‘दैनिक सत्य’ से जुड़ा आम आदमी किसी भी क्षण योद्धा बन सकता है।
समानता के लिये किया गया कोई भी प्रयत्न या आन्दोलन स्वागत के योग्य हैं, चाहे वह शासन की तरफ से हो या आम आदमी की तरफ से।
सामाजिक स्तर पर व्यक्ति की समानता एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अब हम उस अगली समानता पर आते हैं, जो हर स्तर पर अपना होना जताती है और जिसके द्वारा बुनियादी तौर पर उस समानता को स्थापित किया जा सकता है जो किसी भी विषमता से न केवल टक्कर ले सकता है, बल्कि बड़ी आसानी से उसे अपने में जब्ज भी कर सकती है। कोई सुन्दर पक्ष भी जब अपने मूल से विच्छिन्न होकर अपने को स्थापित करना चाहता है, तब वह कोई परिणाम प्रस्तुत करने के बावजूद एक तात्कालिक प्रयोजन होकर रह जाता है।
आज रोटी की तलाश में एक आदमी की पूरी जिन्दगी पार हो जाती है। अगली खोजों का कोई नक्शा उसके जेहन में नहीं उभरता है—उभरता भी है तो वह अपनी उसी क्षण की जरूरतों से इतना आक्रान्त है कि उन ‘सूर्यमुखा यात्राओं’ के बारे में सोचने का उसके पास वक्त ही नहीं है, न शक्ति है और न तैयारी ही।
जब हम मनुष्य के अधिकारों के बारे में सोचते हैं तो एक ही शब्द सामने आकर ठहर जाता है, वह है ‘स्वतन्त्रता’। जागतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से यह मनुष्य का सर्वप्रथम अधिकार है या सबसे बड़ी ज़रूरत। सांसारिक दृष्टि से हमने इसे काफी दूर तक समझने का प्रयत्न किया है, पर आत्मिक स्तर पर इसे ‘स्वतन्त्रभाव’ के रूप में जाना गया है—हर स्थिति परिस्थिति, सुख-दुख रोग-शोक से परे रहनेवाला एक ‘भाव’, या इनके बीच रहते हुए भी इनसे सर्वथा स्वाधीन रहनेवाला भाव।
इस प्रथम अधिकार को संकुचित अर्थ में ‘समानता से भी परिभाषित किया जा सकता है। जब हम ‘रोटी’ की बात करते हैं तब वह आर्थिक समानता को प्रकट करने वाला तथ्य होती है, एक प्रतीक जिसका सम्बन्ध मनुष्य के दैनिक जीवन के हर क्षण से है। और जब हम ‘मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है’ की बात करते हैं, तब वह मनुष्य की जरूरतों पर लगनेवाला बुजुर्वा ताला नहीं, बल्कि दैनिक जीवन से अगली एक स्थिति होती है, जिसे उन उपलब्धियों का आनन्द कहा जा सकता है, जिसे उसने अधिक संघर्षपूर्ण लेकिन श्रेष्ठतर यात्रा-प्रसंगों में पाया है।
अब सवाल यह है कि अपने इस प्रथम अधिकार को सिद्ध करने के लिए मनुष्य उन बाधाओं को कैसे दूर करे, जो बहुत पहली सीढ़ी पर ही उसके कदमों को दबोचकर रखती हैं। समाधान एकपक्षीय नहीं हो सकता और न इसमें कोई समझौतापरक नीति ही काम दे सकती है। जैसी यह दो-टूक समस्या है, वैसा ही दो-टूक इसका हल होना चाहिए। प्रगतिशील वर्ग इसका उत्तर देता है संघर्ष अर्थात् क्रान्ति। क्रान्ति सही और सम्पूर्ण अर्थ में जागरुकता है—एक सच्ची सम्मूर्ण जागरुकता। तब इस जागरूकता का स्वरूप क्या हो और इसे कैसे जन-जन का विषय बनाया जाये—हर जागृति हमें अपनी सीमा से बाहर देखने के लिए विवश करती है और यही उपाय है, जिससे हम अपने समानता और स्वतन्त्रता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अगली प्राप्तियों के लिए दैनिक जीवन की परतन्त्रता की बाधा को नकार सकते हैं।
दुर्भाग्य यह है कि हम अपने दैनिक जीवन के लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने के कारण उन मूल्यों में अपनी आस्था खो बैठे हैं, जो हमें उस परिष्कार में ले जाते हैं, जहाँ हर अगला चरण अधिक प्रकाशमान दुनिया में पड़ता है। एक महत्त्वपूर्ण वर्ग के लिए धर्म-दर्शन, अध्यात्म, संस्कृति आदि शब्द केवल ‘पुरातनता’ के सूचक हैं। परिवारों में ‘धर्म’ शब्द पूजाघरों तक, ‘दर्शन’ शब्द पुस्तकालयों तक और ‘योग-अध्यात्म’ शब्द कुछ मठो की सम्पदा होकर रह गया है, लेकिन जब हम जागरुकता के तहत ‘धर्म’ शब्द की बात करेंगे, तब उसका अर्थ होगा वह आधारशिला, जो किसी भी सद् वस्तु की पीठिका हो सकती है। जब हम ‘दर्शन’ शब्द की बात करेंगे, तब उसका अर्थ होगा वह दृष्टि जो सिर्फ देखती ही नहीं, उन तत्त्वों को भेद कर मार्ग बनाने का काम भी करती है, जिनमें प्रवेश किए बिना ‘देखना’ पूरा नहीं होता। जब हम ‘योग’ की बात करेंगे तो उसका अर्थ होगा ‘समत्व’ का ऐसा आचरण जो ‘कर्म की कुशलता’ और ‘नैष्कर्म्य की सिद्धि’ के लिए जरूरी है। जब ‘अध्यात्म की बात होगी तो उसका अर्थ होगा अपनी बुनियाद में लौटना, जिसे ‘स्वभाव’ कहा जाता है।
हमें जागृति की जरूरत है।
ताकि हम अपने प्रथम अधिकार या पहली जरूरत ‘स्वतन्त्रता’ को अर्जित कर सकें।
‘धर्म’ जैसे ही अपने आवास-स्थान ‘हृद्देशे तिष्ठति’ का त्याग कर मन्दिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, मठों, गुरुद्वारों की दीवारों में अपना अर्थ ध्वनित करने लगता है, वैसे ही वह ‘ग्लानि’ की सीमा में प्रवेश कर जाता है। निश्चित ही धर्म की इस ग्लानि को धर्मेतर किसी विकल्प की प्रतिष्ठा के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म का कोई विकल्प नहीं होता।
हम आधुनिक जन समझौतापरक नीति की खिलाफ़त करके यह सोचने लगते हैं कि प्रगतिशीलता की दौड़ में हम बहुत आगे निकल गये हैं, और जहाँ लोग बीसवीं शताब्दी के इस उत्तरार्ध में भी धर्म, दर्शन और अध्यात्म की बात करने में लगे हुए हैं, वे निहायत रूढ़, बुजदिल और अप्रगतिशील हैं। ऐसा करते हुए हम उस एहसास से मुँह चुराते हैं, जो हमारे लिए एक सत्य लेकिन कठोर क्षण की रचना करता है। वास्तव में हम धार्मिक आदमी के खतरे को नहीं जानते। धार्मिक होने की कठिनता से हम कभी नहीं गुजरे। आध्यात्मिक होने की उस खुली तलवार को हमने कभी नहीं देखा, जो हमें इतना सचेतन रखती है कि हमारी छोटी-से-छोटी एक भूल, हमारा एक नन्हा-सा अपराध हमारे हृदय का रक्त निचोड़ लेता है।
सैद्धान्तिक लड़ाइयों का अपना एक इतिहास रहा है। आज भी वह लड़ाई कई वर्दियों के दरमियान चल रही है। यह लड़ाई सिद्धान्तों की खुली लड़ाई नहीं है, बल्कि अपनी-अपनी मान्यताओं को प्रतिष्ठित करने की लड़ाई है। हमारे भीतर किसी विजयी सिद्धान्त को स्वीकार करने की मनोवृत्ति नहीं है, बल्कि हम उसी मान्यता को प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, जिसके होने से हमारी निजी शक्ति बढ़ती है। अब ‘मण्डन मिश्र’ नहीं रहे जो हारकर पराजय और कुण्ठा का शिकार नहीं हुए थे, बल्कि उस ऊँचाई के प्रति विनत हुए थे, जो शंकराचार्य थे। अब विजय में सत्य को स्थापित कर पाने का सुख नहीं है, अब हार में कुछ और आगे जा पाने की उत्कण्ठा नहीं है।
पर यह ‘नहीं’ ‘नास्ति’ नहीं है, क्योंकि जो होता है, वह रहता ही है। यह ‘नास्ति’ सिर्फ एक ऊपरी इन्कार है क्योंकि स्वीकृति का सम्बन्ध किसी दूरस्थ ऊँचाई से नहीं है, बल्कि गहराई से है—कम-से-कम अपेक्षाकृत रूप से। यदि हम एक क्षण के लिए भी अपने अन्दर की गहराई में उतर सकें, तो शाश्वत मूल्यों के प्रति वहाँ एक सहज स्वीकार हम स्पष्ट अनुभव करेंगे। प्रगतिशील जन यह न भूलें कि उनके अपने कितने ही पड़ाव ऐसे हैं, जहाँ समझौते ने अपने तम्बू तान रखे हैं।.....जब यह बात कही गई कि ‘धर्म का कोई विकल्प नहीं होता’, तब कहना यह भी चाहा था कि ‘धर्म’ अत्यन्त सहिष्णु होकर भी समझौतापरक नहीं होता। वह अपने आदर्श, आचार, आस्था, निष्ठा और भाव के सामने, अपने ईश्वर के सामने अन्य किसी प्रतिआदर्श, तत्त्व या विचार को स्वीकार नहीं करता। ‘यथास्थान’ होने और देखने में उसका विश्वास है, इसलिए वह किसी भी ‘परता’ के प्रति सहिष्णु और उदार होता है, पर उसे ‘अन्तर्गत’ नहीं लेता। धर्म जब संस्कृति के रूप में अन्य किसी तत्त्व या अनेक तत्त्वों को आत्मसात् करता है, तब इन तत्त्वों में कहीं-न-कहीं कोई संगति अवश्य होती है।
धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन कहीं न कहीं एक हो जाते हैं, या कहें ‘धर्म’ अपने शुद्धतम् अर्थ में ‘अध्यात्म से जुड़ जाता है। इन दोनों का ही कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गों पर चलनेवालों के लिए भी कोई विकल्प नहीं रह जाता। ईसा हों या मन्सूर मस्तान, उनका लक्ष्य ही उनकी नियति होती है।
सत्य के आचरण और प्रतिष्ठा के लिए जरूरी है कि हम ‘धार्मिक पुरुष’ की तरह व्यवहार करें और ‘समझौतों’ के नाम पर उन ‘विकल्पों’ को स्वीकार न करें जिनके अन्दर एक स्वाभाविक विरोध या द्वन्द्वभाव है। ‘आरोपित विरोध’ को सहन किया जा सकता है, उसके साथ कोशिश की जा सकती है, उसमें बदलाव लाया जा सकता है—क्योंकि कहीं न कहीं उसमें कोई न कोई तत्त्व संगतिपूर्ण खोजा जा सकता है। ‘स्वाभाविक विरोध और द्वन्द्व’ से सुलटने के दो रास्ते हैं—समय की प्रतीक्षा करना, क्योंकि कालान्तर में उनका विघटन और विसर्जन निश्चित है; और निरन्तर संघर्षशील रहते हुए ऐसे प्रति-तत्त्वों का निरन्तर क्षीण करते जाना।
प्रायः समझौते का अर्थ होता है, किसी ‘सत्ता’ के साथ वह स्वीकृति या सहमति, जो हमें अपनी मान्यताओं से हटकर करनी पड़ती है। यदि हमारी मान्यता ‘स्वधर्म’ से जुड़ी है, तब तो यह स्वीकृति हमारे मौलिक और प्राथमिक व्यक्तित्व को ही खतरे में डाल देगी और हम विघटन का शिकार हो जायेंगे। इसलिए ‘समझौता’ हो या विरोध—इन दोनों को ही ‘स्व’ और ‘पर’ के पलट पर देख-जाँच कर उठाया जानेवाला कदम ही जागरुक कदम होगा, हमारी जागृति का सूचक होगा।षय्गन।
पर, लिखा गया हर शब्द सिर्फ सामयिक नहीं होता, वह समय की चेतना को स्पर्श करता हुआ उससे आगे भी जाता है।
शायद इन पृष्ठों में ऐसा हुआ हो।
जीवन और जगत् की दिशा में जब भी हमने सोचने की कोशिश की, हमेशा एक टकराहट का सामना करना पड़ा। दरअसल प्रश्न इतने ज्यादा हैं और समाधान इतने कम की चीजें विरोधी रूप धारण करके अपने हल की दिशा में बढ़ने के बजाए आपस में ही टकराने लगती हैं। इस टकराहट को संघर्ष कहना, और वह भी सृजनशील संघर्ष कहना, जरा भी मुनासिब नहीं होगा। संघर्ष एक जागरुक प्रयत्न है जिसका उद्देश्य निश्चित और स्पष्ट है होता है। धर्म के नाम पर हो या आध्यात्मिकता के नाम पर, परम्परा के नाम पर हो या आधुनिकता के नाम पर, प्रगतिशीलता हो या प्रतिक्रियाशीलता, कोई भी अन्धा प्रयत्न संघर्ष नहीं कर सकता, और इसलिए वह कभी भी क्रान्ति में, एक सफल और निश्चित परिणामवाली क्रान्ति में नहीं ढल सकता।
आज रास्ता चलते हम हवाओं में गर्मी महसूस करते हैं। तापमान हर रोज बढ़ रहा है और साथ ही भारीपन भी। यह हवाओं में छुपी हुई उस आग का सूचक है, जो किसी भी क्षण विस्फोट का रुप ले सकती है। हम सब इस सम्भावित विस्फोट के नीचे खड़े हैं। हमारे अपने ही नष्ट हो जाने का खतरा है। अगर हम इस आग को वैदिक ऋषि के सदृश्य सृष्टि की ऋचा की तरह नहीं रच सके, तो हमें उस नुकसान को सहन करना पड़ेगा जो देखने में लपट को ऊँची करने का प्रयत्न लगता है, लेकिन जो सिर्फ धुआँ होकर रह जाता है। हमें इस आग को अपने अग्रणी क्रान्ति-पुरुष का मस्तक बनाना है। इसे वह स्वरूप देना है, जिसमें हम अपनी वास्तविक दुनिया का दर्शन कर सकेंगे। हमें इस अग्नि की उज्ज्वलता में से वह मेधा बटोरनी है, जिससे युक्त होकर हम अपने झितिजों को अन्धकारमुक्त कर सकेंगे। यह सही है कि आग है और वह हवाओं की मर्जी पर किसी भी दिशा में तेजी पकड़ सकती है, पर आग को हिलाने से पहले क्या यह जरूरी नहीं है कि हम हवाओं को वह रुख दें, जो हमारा अपना रुख हो, हमारी अपनी दिशा। जब तक हिन्दुस्तान की आँखें अपनी नासिका के अग्रभाग पर केन्दित नहीं होंगी तब तक वह पराये प्रभावों के कुचक्र में फँसा रहेगा। गीता का अपने से अपने को देखना ‘आत्मनात्मानं पश्येत्’ और बुद्ध का ‘अप्पदीपो भव’ उपदेश इसी ज्ञान का निर्णय करते हैं। इस सन्दर्भ में यह दोहराना जरूरी है कि हमें अपना लक्ष्यभेद अपने ही तीर से करना होगा।
अगर हमें क्रांति के बीजों को हिन्दुस्तान की धरती पर बोना है तो पहले इस धरती के चरित्र को पहचान लेना होगा। इस भूमि ने उन बीजों को भी कभी अंकुरित नहीं किया जो इसके निजी व्यक्तित्व या स्वधर्म के विरुद्ध पड़ते हैं। अपनी स्वाभाविक करुणा से इसने उनका विनाश भले ही किया हो, पर ज्यों का त्यों वमन जरूर कर दिया। इस वमन के पीछे उन कारणों को तलाशना व्यर्थ होगा, जो धरती को अनुर्वरा घोषित करते हैं और उस खाद को भी डालना व्यर्थ होगा, जो भूमि के निजी गुण का हनन कर इन बीजों को प्रतिफलित करने में मदद करती है। हमें वह फसल उगानी होगी जो हमेशा ही हमें पुष्ट और सबल बनाती रही है। इस दृष्टि से हमें सिर्फ सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक क्रान्ति से ही नहीं गुजरना, बल्कि धर्म, दर्शन, संस्कृति, कला और अध्यात्म की दिशा में भी रूपान्तरण प्रस्तुत करना है। उन सब मूल्यों को साथ लेकर चलना है, जिनसे भारतीय मानस अभिच्छेद्य रूप से जुड़ा है। एक तरफ हमें अनास्था, सतही बौद्धिकता, अकर्मण्य प्रगतिशीलता और निष्प्रेम विद्रोह के बुलबुलों को फोड़ना है तो दूसरी तरफ अन्धविश्वास, आडम्बर और तथाकथित गुरुओं की बढ़ती हुई भीड़ में से जागरुक विश्वास, सत्यनिष्ठा और उस ‘नेतृत्व’ को तलाशना है, जो न केवल हमारे जागतिक व्यक्तित्व और स्वातन्त्र्य के लिए, बल्कि हमारी आत्मा के लिए भी प्रसिद्ध हो।
जब हम आत्मिक प्रतिबद्धता की बात करते हैं, तब अन्य कोई भी पक्ष अप्रतिश्रुति नहीं रह जाता। वास्तव में सम्पूर्ण दायित्व और सम्पूर्ण स्वीकार अथवा सम्पूर्णता मात्र ही आध्यात्मिक जीवन का यात्रा-प्रसंग है।
विश्व के सभी धर्मग्रन्थों में यह प्रतिबद्धता निश्चित भाषा में प्रकट हुई है। श्रीकृष्ण की अर्जुन के प्रति की गयी यह प्रतिज्ञा—‘मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे’ मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मुझे ही प्राप्त होगा, तू मुझे प्रिय है—आगे और भी स्पष्ट हो जाती है, जब वे कहते हैं ‘अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः’— मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूँगा, तू चिन्ता मत कर। ये शब्द किसी भी पूर्वापरता से स्वतन्त्र अपने परिणाम में स्वयं समर्थ हैं, क्योंकि भगवदीय वचनों की सार्थकता किसी भी ‘पर’ पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। लेकिन इस तथ्य की विषद व्याख्या हमारा प्रस्तुत प्रसंग न होने के कारण हम उन वाक्यों के बारे में सोचते हैं, जो इस प्रतिश्रुति में शर्त की तरह ध्वनित होते हैं।
‘मुझमें अपना मन लगा’ मेरा भक्त बन, मुझे नमन कर, एक मात्र मेरी शरण में आ’ मानो ये सब अपेक्षायें पूरी किये बगैर वह प्रतिज्ञा एक कमजोर आश्वासन मात्र रह जाती है। इसी तरह ‘परशुराम-कल्पशूत्र’ का यह शूत्र ‘अनुग्रहः
संश्रितेषु—आश्रितों को भगवदीय कृपा प्राप्त होती है—एक शर्त है, क्योंकि कृपा मुक्त नहीं है, ‘आश्रय-भाव’ में बद्ध है। बुद्ध ने भी बार-बार कहा है ‘बुद्ध की शरण में आ, धर्म की शरण में, संघ की शरण आ, दुःखों का निवारण तभी हो सकेगा। ‘ईसा ने कहा’, ‘जो मेरे पास आयेगा, उसके सब पाप क्षमा कर दिये जायेंगे, जो मेरा विश्वास करेगा, वह स्वर्ग के साम्राज्य में प्रवेश पायेगा।’ इन सब भगवद पुरुषों के ये कथन उस प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं, जो अपने निजी नियमों में चलती है या अपने प्रतिफल के लिए दूसरे पक्ष में एक विशिष्ट स्थिति की या मनोवृत्ति की माँग करती है। इसलिए प्रतिबद्धता सिर्फ शरणागत के लिए होने के कारण व्यक्तिपरक होकर रह जाती है। यह व्यक्ति के लिए ऐकान्तिक कल्याण का प्रतीक है, समाज से जिसका कोई प्रकट और समर्थ सम्बन्ध नहीं है।
तो क्या हम यह विश्वास करें कि भगवदीय प्रेम और व्यक्ति की निष्कृति इस सापेक्ष सम्बन्ध में निहित है ?
वस्तुतः यह प्रतिज्ञा व्यक्ति और भगवान् के बीच के निजी सम्बन्ध की सूचक है, जो सम्बन्ध काफी लम्बी आत्मिक यात्रा के बाद सिद्ध होता है। अब हम उस प्रतिज्ञा की बात करेंगे, गीता ने जिसे अत्यन्त व्यापक या वैश्विक सन्दर्भ में प्रकट किया है, और ‘अवतारवाद’ सिद्धान्त के विचार-विमर्श में जिसका मामूली अनपढ़ व्यक्ति और प्रकाण्ड पण्डित एक साथ करता है ‘यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ! अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।’—इस सन्दर्भ में हम किसी अवतरण की व्याख्या न कर, उस प्रतिबद्ध पुरुष के जन्म की बात करेंगे, जो सचमुच ही अपने इस वचन को निभाने में समर्थ है। ‘धर्म की ग्लानि’ मानव-जीवन के उन आन्तरिक मूल्यों का पतन, है जो उसे मनुष्य होने के सौन्दर्य-गुण से मण्डित करते हैं। कोई भी विघटन धर्म की इस सुद़ढ़ आधारशिला की टूटन ही है। जीवन के वे मूल्य, जो ‘अस्ति’ भाव के प्रतीक हैं, जब धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक साहित्यक और सांस्कृतिक क्षेत्र में तथा सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत सम्बन्धों की दिशा में अपना वजन खो बैठते हैं, वहीं से ‘धर्म की ग्लानि’ शुरू हो जाती है। उस ‘अस्ति’ भाव की प्रतिष्ठा इस प्रतिज्ञात पुरुष के जन्म के कारण बनती है। पहली प्रतिज्ञा की तरह यह दूसरी प्रतिज्ञा सृष्टि के प्रथम दिनारम्भ से अब तक अपने तदर्थ में ज्यों की त्यों बनी हुई है।
इसी प्रतिज्ञा का दूसरा भाग है, ‘परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्’— साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए मैं अपने को रचता हूँ। साधुजन सिर्फ ईश्वरवादी लोग ही नहीं, वे निरीह सज्जन प्राणी भी हैं, जो अपने छोटे-छोटे सत्यों को अब भी अपने हृदय से लगाये निरन्तर संघर्षरत हैं। किसी बड़े दार्शनिक या वैचारिक या बौधिक सत्य का चेहरा इन्होंने भले ही न देखा हो, लेकिन जो अपनी नन्हीं आस्थाओं के बल पर अब भी हर सुबह उगते हुए सूर्य को ‘मित्र’ कहकर सम्बोधित करते हैं। इन निरीह कोमल प्राणियों की रक्षा ईश्वर का निजी कृत्य है या कहें दायित्व है, जिसके लिए सीधी सरल ‘साधुता’ के अतिरिक्त अन्य कोई अपेक्षा नहीं है।
लेकिन उपर्युक्त वाक्य के उत्तरार्ध में एक तीसरी प्रतिज्ञा या प्रतिबद्धता है दुर्जनों के लिए। ‘निरवैरः सर्वेभूतेषु यः स मामेति पाण्डव’—जो सब प्राणियों में वैररहित है, वह मुझे प्राप्त करता है यह जिसकी प्राप्ति की शर्त है, वह स्वयं ‘दुर्जन’ के प्रति कैसे वैर रख सकता है ? उसका उनके प्रति भी उसी तत्परता से प्रतिबद्ध होना उसके अपने चरित्र की अनिवार्यता है। जो दुष्ट हैं, पापी है, दरिद्र हैं, मलिन हैं, अन्यायी और अत्याचारी हैं, निष्प्रेम और निष्करुण हैं, वे उसके अपने शरीर का व्रण हैं।
वह इस ‘व्रण’ का उपचार कई तरह से करता है, कभी औषधि कभी प्रलेप द्वारा, कभी शल्य द्वारा। जब वह दुर्जनों के विनाश की बात करता है, तब साधुओं के परित्राण की सापेक्षता के कारण नहीं, स्वयं दुर्जनों को उनकी ‘कर्दम-कृमिता’ से उबार लेने के लिए, जिसमें वे संस्कारगत रूप में पड़े हुए हैं। दुर्जनों का यह विनाश या हिंसा द्वेषप्रेरित नहीं है, ठीक उसी प्रेम और करुणा का आयोजन है, जिससे वह साधुओं के परित्राण के लिए प्रेरित होता है। महाभारत युद्ध की रंग-रचना करनेवाले श्रीकृष्ण किसी व्यक्ति, जाति, समाज अथवा पक्ष के हित या अहित में इस युद्ध के सूत्रधार नहीं हैं, बल्कि पृथ्वी पर अपने होने की प्रतिज्ञा के पीछे जो कारण है, उसकी सिद्धि के लिए ही इस रक्त-अनुष्ठान की रचना करते हैं।
तो क्या हम धर्म के प्रति, साधु के प्रति, दुर्जन के प्रति, विश्व की चतुर्मूर्ति के प्रति प्रतिबद्ध इस पुरुष की प्रतीक्षा करें या राष्ट्र के हृदय की दबी हुई आग में इस ‘हृत्पुरुष’ का जन्म हो चुका है ?
समाज और व्यक्ति-व्यक्ति के बीच की विषमताओं और विभेदताओं के हल करने के लिए यह जरूरी है कि शासन इस विभेद को मिटाये और एक समान व्यवस्था को कायम करे। इस विषमता और विभेद की रचना करने वालों की संख्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इन ‘व्यक्ति विशेषों’ के साथ आम आदमी की बहुत बड़ी संख्या भी जुड़ी हुई है, जो इस खाई को गहरा और चौड़ा करने के लिए अपने हाथ में कुदाली, फावड़ा लिए खड़ी है। यह आम आदमी अपने दैनिक सत्य (रोटी) के लिए महत्तर सत्य के प्रति विमुख रहने के लिए विवश है, जो यह कहता है ‘मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है।’
खाई के वे रबर-सिरे किसी भी क्षण उन लोगों से छीने जा सकते हैं जो इसे लगातार खींचते जा रहे हैं और ‘दैनिक सत्य’ से जुड़ा आम आदमी किसी भी क्षण योद्धा बन सकता है।
समानता के लिये किया गया कोई भी प्रयत्न या आन्दोलन स्वागत के योग्य हैं, चाहे वह शासन की तरफ से हो या आम आदमी की तरफ से।
सामाजिक स्तर पर व्यक्ति की समानता एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अब हम उस अगली समानता पर आते हैं, जो हर स्तर पर अपना होना जताती है और जिसके द्वारा बुनियादी तौर पर उस समानता को स्थापित किया जा सकता है जो किसी भी विषमता से न केवल टक्कर ले सकता है, बल्कि बड़ी आसानी से उसे अपने में जब्ज भी कर सकती है। कोई सुन्दर पक्ष भी जब अपने मूल से विच्छिन्न होकर अपने को स्थापित करना चाहता है, तब वह कोई परिणाम प्रस्तुत करने के बावजूद एक तात्कालिक प्रयोजन होकर रह जाता है।
आज रोटी की तलाश में एक आदमी की पूरी जिन्दगी पार हो जाती है। अगली खोजों का कोई नक्शा उसके जेहन में नहीं उभरता है—उभरता भी है तो वह अपनी उसी क्षण की जरूरतों से इतना आक्रान्त है कि उन ‘सूर्यमुखा यात्राओं’ के बारे में सोचने का उसके पास वक्त ही नहीं है, न शक्ति है और न तैयारी ही।
जब हम मनुष्य के अधिकारों के बारे में सोचते हैं तो एक ही शब्द सामने आकर ठहर जाता है, वह है ‘स्वतन्त्रता’। जागतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से यह मनुष्य का सर्वप्रथम अधिकार है या सबसे बड़ी ज़रूरत। सांसारिक दृष्टि से हमने इसे काफी दूर तक समझने का प्रयत्न किया है, पर आत्मिक स्तर पर इसे ‘स्वतन्त्रभाव’ के रूप में जाना गया है—हर स्थिति परिस्थिति, सुख-दुख रोग-शोक से परे रहनेवाला एक ‘भाव’, या इनके बीच रहते हुए भी इनसे सर्वथा स्वाधीन रहनेवाला भाव।
इस प्रथम अधिकार को संकुचित अर्थ में ‘समानता से भी परिभाषित किया जा सकता है। जब हम ‘रोटी’ की बात करते हैं तब वह आर्थिक समानता को प्रकट करने वाला तथ्य होती है, एक प्रतीक जिसका सम्बन्ध मनुष्य के दैनिक जीवन के हर क्षण से है। और जब हम ‘मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है’ की बात करते हैं, तब वह मनुष्य की जरूरतों पर लगनेवाला बुजुर्वा ताला नहीं, बल्कि दैनिक जीवन से अगली एक स्थिति होती है, जिसे उन उपलब्धियों का आनन्द कहा जा सकता है, जिसे उसने अधिक संघर्षपूर्ण लेकिन श्रेष्ठतर यात्रा-प्रसंगों में पाया है।
अब सवाल यह है कि अपने इस प्रथम अधिकार को सिद्ध करने के लिए मनुष्य उन बाधाओं को कैसे दूर करे, जो बहुत पहली सीढ़ी पर ही उसके कदमों को दबोचकर रखती हैं। समाधान एकपक्षीय नहीं हो सकता और न इसमें कोई समझौतापरक नीति ही काम दे सकती है। जैसी यह दो-टूक समस्या है, वैसा ही दो-टूक इसका हल होना चाहिए। प्रगतिशील वर्ग इसका उत्तर देता है संघर्ष अर्थात् क्रान्ति। क्रान्ति सही और सम्पूर्ण अर्थ में जागरुकता है—एक सच्ची सम्मूर्ण जागरुकता। तब इस जागरूकता का स्वरूप क्या हो और इसे कैसे जन-जन का विषय बनाया जाये—हर जागृति हमें अपनी सीमा से बाहर देखने के लिए विवश करती है और यही उपाय है, जिससे हम अपने समानता और स्वतन्त्रता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अगली प्राप्तियों के लिए दैनिक जीवन की परतन्त्रता की बाधा को नकार सकते हैं।
दुर्भाग्य यह है कि हम अपने दैनिक जीवन के लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने के कारण उन मूल्यों में अपनी आस्था खो बैठे हैं, जो हमें उस परिष्कार में ले जाते हैं, जहाँ हर अगला चरण अधिक प्रकाशमान दुनिया में पड़ता है। एक महत्त्वपूर्ण वर्ग के लिए धर्म-दर्शन, अध्यात्म, संस्कृति आदि शब्द केवल ‘पुरातनता’ के सूचक हैं। परिवारों में ‘धर्म’ शब्द पूजाघरों तक, ‘दर्शन’ शब्द पुस्तकालयों तक और ‘योग-अध्यात्म’ शब्द कुछ मठो की सम्पदा होकर रह गया है, लेकिन जब हम जागरुकता के तहत ‘धर्म’ शब्द की बात करेंगे, तब उसका अर्थ होगा वह आधारशिला, जो किसी भी सद् वस्तु की पीठिका हो सकती है। जब हम ‘दर्शन’ शब्द की बात करेंगे, तब उसका अर्थ होगा वह दृष्टि जो सिर्फ देखती ही नहीं, उन तत्त्वों को भेद कर मार्ग बनाने का काम भी करती है, जिनमें प्रवेश किए बिना ‘देखना’ पूरा नहीं होता। जब हम ‘योग’ की बात करेंगे तो उसका अर्थ होगा ‘समत्व’ का ऐसा आचरण जो ‘कर्म की कुशलता’ और ‘नैष्कर्म्य की सिद्धि’ के लिए जरूरी है। जब ‘अध्यात्म की बात होगी तो उसका अर्थ होगा अपनी बुनियाद में लौटना, जिसे ‘स्वभाव’ कहा जाता है।
हमें जागृति की जरूरत है।
ताकि हम अपने प्रथम अधिकार या पहली जरूरत ‘स्वतन्त्रता’ को अर्जित कर सकें।
‘धर्म’ जैसे ही अपने आवास-स्थान ‘हृद्देशे तिष्ठति’ का त्याग कर मन्दिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, मठों, गुरुद्वारों की दीवारों में अपना अर्थ ध्वनित करने लगता है, वैसे ही वह ‘ग्लानि’ की सीमा में प्रवेश कर जाता है। निश्चित ही धर्म की इस ग्लानि को धर्मेतर किसी विकल्प की प्रतिष्ठा के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म का कोई विकल्प नहीं होता।
हम आधुनिक जन समझौतापरक नीति की खिलाफ़त करके यह सोचने लगते हैं कि प्रगतिशीलता की दौड़ में हम बहुत आगे निकल गये हैं, और जहाँ लोग बीसवीं शताब्दी के इस उत्तरार्ध में भी धर्म, दर्शन और अध्यात्म की बात करने में लगे हुए हैं, वे निहायत रूढ़, बुजदिल और अप्रगतिशील हैं। ऐसा करते हुए हम उस एहसास से मुँह चुराते हैं, जो हमारे लिए एक सत्य लेकिन कठोर क्षण की रचना करता है। वास्तव में हम धार्मिक आदमी के खतरे को नहीं जानते। धार्मिक होने की कठिनता से हम कभी नहीं गुजरे। आध्यात्मिक होने की उस खुली तलवार को हमने कभी नहीं देखा, जो हमें इतना सचेतन रखती है कि हमारी छोटी-से-छोटी एक भूल, हमारा एक नन्हा-सा अपराध हमारे हृदय का रक्त निचोड़ लेता है।
सैद्धान्तिक लड़ाइयों का अपना एक इतिहास रहा है। आज भी वह लड़ाई कई वर्दियों के दरमियान चल रही है। यह लड़ाई सिद्धान्तों की खुली लड़ाई नहीं है, बल्कि अपनी-अपनी मान्यताओं को प्रतिष्ठित करने की लड़ाई है। हमारे भीतर किसी विजयी सिद्धान्त को स्वीकार करने की मनोवृत्ति नहीं है, बल्कि हम उसी मान्यता को प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, जिसके होने से हमारी निजी शक्ति बढ़ती है। अब ‘मण्डन मिश्र’ नहीं रहे जो हारकर पराजय और कुण्ठा का शिकार नहीं हुए थे, बल्कि उस ऊँचाई के प्रति विनत हुए थे, जो शंकराचार्य थे। अब विजय में सत्य को स्थापित कर पाने का सुख नहीं है, अब हार में कुछ और आगे जा पाने की उत्कण्ठा नहीं है।
पर यह ‘नहीं’ ‘नास्ति’ नहीं है, क्योंकि जो होता है, वह रहता ही है। यह ‘नास्ति’ सिर्फ एक ऊपरी इन्कार है क्योंकि स्वीकृति का सम्बन्ध किसी दूरस्थ ऊँचाई से नहीं है, बल्कि गहराई से है—कम-से-कम अपेक्षाकृत रूप से। यदि हम एक क्षण के लिए भी अपने अन्दर की गहराई में उतर सकें, तो शाश्वत मूल्यों के प्रति वहाँ एक सहज स्वीकार हम स्पष्ट अनुभव करेंगे। प्रगतिशील जन यह न भूलें कि उनके अपने कितने ही पड़ाव ऐसे हैं, जहाँ समझौते ने अपने तम्बू तान रखे हैं।.....जब यह बात कही गई कि ‘धर्म का कोई विकल्प नहीं होता’, तब कहना यह भी चाहा था कि ‘धर्म’ अत्यन्त सहिष्णु होकर भी समझौतापरक नहीं होता। वह अपने आदर्श, आचार, आस्था, निष्ठा और भाव के सामने, अपने ईश्वर के सामने अन्य किसी प्रतिआदर्श, तत्त्व या विचार को स्वीकार नहीं करता। ‘यथास्थान’ होने और देखने में उसका विश्वास है, इसलिए वह किसी भी ‘परता’ के प्रति सहिष्णु और उदार होता है, पर उसे ‘अन्तर्गत’ नहीं लेता। धर्म जब संस्कृति के रूप में अन्य किसी तत्त्व या अनेक तत्त्वों को आत्मसात् करता है, तब इन तत्त्वों में कहीं-न-कहीं कोई संगति अवश्य होती है।
धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन कहीं न कहीं एक हो जाते हैं, या कहें ‘धर्म’ अपने शुद्धतम् अर्थ में ‘अध्यात्म से जुड़ जाता है। इन दोनों का ही कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गों पर चलनेवालों के लिए भी कोई विकल्प नहीं रह जाता। ईसा हों या मन्सूर मस्तान, उनका लक्ष्य ही उनकी नियति होती है।
सत्य के आचरण और प्रतिष्ठा के लिए जरूरी है कि हम ‘धार्मिक पुरुष’ की तरह व्यवहार करें और ‘समझौतों’ के नाम पर उन ‘विकल्पों’ को स्वीकार न करें जिनके अन्दर एक स्वाभाविक विरोध या द्वन्द्वभाव है। ‘आरोपित विरोध’ को सहन किया जा सकता है, उसके साथ कोशिश की जा सकती है, उसमें बदलाव लाया जा सकता है—क्योंकि कहीं न कहीं उसमें कोई न कोई तत्त्व संगतिपूर्ण खोजा जा सकता है। ‘स्वाभाविक विरोध और द्वन्द्व’ से सुलटने के दो रास्ते हैं—समय की प्रतीक्षा करना, क्योंकि कालान्तर में उनका विघटन और विसर्जन निश्चित है; और निरन्तर संघर्षशील रहते हुए ऐसे प्रति-तत्त्वों का निरन्तर क्षीण करते जाना।
प्रायः समझौते का अर्थ होता है, किसी ‘सत्ता’ के साथ वह स्वीकृति या सहमति, जो हमें अपनी मान्यताओं से हटकर करनी पड़ती है। यदि हमारी मान्यता ‘स्वधर्म’ से जुड़ी है, तब तो यह स्वीकृति हमारे मौलिक और प्राथमिक व्यक्तित्व को ही खतरे में डाल देगी और हम विघटन का शिकार हो जायेंगे। इसलिए ‘समझौता’ हो या विरोध—इन दोनों को ही ‘स्व’ और ‘पर’ के पलट पर देख-जाँच कर उठाया जानेवाला कदम ही जागरुक कदम होगा, हमारी जागृति का सूचक होगा।षय्गन।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book