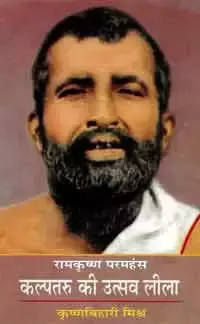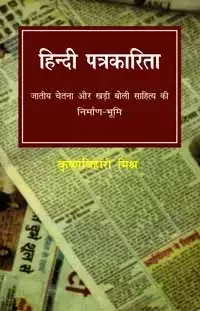|
लेख-निबंध >> नेह के नाते अनेक नेह के नाते अनेककृष्णबिहारी मिश्र
|
271 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत है नेह के नाते अनेक...
Neh Ke Nate Anek
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
वर्तमान और भविष्य को काफी हद तक आश्वस्त करने वाले, संकटों से घिरी सृजनशील ऊर्जा की याद को ताज़ा करते, इन संस्मरणों में लेखक ने विरासत के मार्मिक तथ्यों के माध्यम से कुछ तीखे सवाल भी खड़े किये हैं। जो नये विमर्श के लिए मूल्यवान सूत्र सिद्ध हो सकते हैं।
भूमिका
हँसमुख साँझ
कमियाँ तब भी थीं जिस समय के चरित्रों के चित्र इन निबन्धों में हैं, मगर सद्भाव के दारिद्रय का आज जैसा अनुभव पहले के समय ने शायद नहीं किया था। वर्तमान संस्कारहीन समय की संवेदना-रिक्तता के त्रासद परिदृश्य से आहत लोगों को अतीत में केवल उज्ज्वलता ही दिखाई पड़े तो यह अस्वाभाविक तो नहीं है, पर ‘सुधा’ के दिसम्बर, 1930 के अंक में बड़ी वेदना और क्षोभ के साथ निराला ने लिखा था-‘‘हिन्दी में तृप्ति की साँस लेते हुए साहित्य-सेवा करनेवाले जितने लोग दीख पड़ते हैं, अधिकांश स्पष्टवादिता से बाहर केवल दलबन्दी के बल पर साहित्य का उद्धार करने वाले चाचा-भतीजे हैं।...यह साहित्य के क्षेत्र में महाअधम कार्य है। करीब-करीब सभी इस तरह की हरकत ताड़ जाते हैं। पर समय कुछ ऐसा है कि जमात ठगों की ही ज़ोरदार है। भले आदमियों को कोई पूछता नहीं।
साहित्य के मशहूर लण्ठ आचार्य माने जाते हैं- हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ लेखक।’’ स्पष्ट है कि अपने समय से शिकायत पहले भी उन तमाम लोगों को थी, जो मूल्यों के पक्षधर थे, साधना के पक्षधर, अगवाह राह के राही नहीं और जो व्यवस्था-प्रवीण लोगों के उन्नत हो रहे वर्चस्व को लक्ष्य कर निराला की तरह दुःखी थे। तथ्य है कि दूध से धुले लोगों की वह पीढ़ी नहीं थी, श्यामता का गहरा स्पर्श आदर्श के राग में जीने वाला समय भी ढो रहा था, अभिशाप के रूप में। श्री रामनाथ ‘सुमन’, पाण्डेय बेचन शर्मा ‘उग्र’ और राय कृष्णदास के संस्मरण इसी तथ्य की सम्पुष्टि करनेवाले साक्ष्य हैं। जो बड़ी बात थी उस पीढ़ी के साथ वह उनका सृजनशील जीवन था, जो समय की चुनौतियों को पीठ न दिखाकर अपनी जुझारू साधना से आनेवाले लोगों के लिए राह बना रहा था;
समय के लिए रोशनी रच रहा था।
यथार्थ के नाम पर कालिख-कलुष बटोरना–परोसना शिविर-विशेष द्वारा प्रगतिशील भूमिका मानी जा सकती है, पर हमें तलाश रहती है उस उज्ज्वल रोशनी की जो विचलित कर देनेवाले झंझावातों का मुक़ाबला करते खँडहरों में दबे दीये की बाती बनकर जल रही होती है, समय को तमस में हम विरासत के पन्नों को उलटते-पलटते हैं। राख के लिए नहीं, ऊष्मा के लिए हम साहित्य से जुड़ते हैं ताकि ठिठुरती-पथराती संवेदना टाँठ और गत्वर हो सके।
बुढ़ौती लोकयात्रा का ऐसा संवेदनशील पड़ाव है, जिसे स्पर्श करते ही व्यतीत की सुधि तीव्र हो जाती है। बूढ़ी साँझ सामान्यतः उदास होती है। और सुधि में सीझना बूढ़ों की नियति बन जाती है, यह उदास ही नहीं बन जाती है, यह अनुभवी बताते हैं। मगर साँझ-वेला में अकसर जागनेवाली सुधि केवल उदास ही नहीं बनाती, उस लोक से भी मन को जोड़ती है, जिसने हमारे जीवन-अनुशासन को रचा है और जागतिक अन्धड़ से पंजा लड़ाने की कला सिखायी है। अपने व्यतीत की पड़ताल करते उन परिदृश्यों, चेहरे-चरित्रों की बरबस याद आती है, जो हमारे सपने थे, अपने थे और जिनके अन्तरंग सान्निध्य में साँस लेते विकट प्रत्यूहों से टकरा-टकराकर हम अपनी ज़मीन तैयार करते रहे हैं।
अतीत-स्मृति का आस्वाद वर्तमान के स्वाद को हर समय फ़ीका नहीं करता, म्लान पड़ रही जीवन-प्रियता को रससिक्त कर पुनर्नवा भी करता है। और तब हम अपने सौभाग्य का साक्षात्कार कर साँझ की हँसमुख मुद्रा की सहज प्रेरणा से अवसाद की आँच में सीझने से स्वयं को बचा पाते हैं। सृजनशील ऊर्जा की रक्षा ही स्व की सुरक्षा की समुचित विधि है। कृती पुरुषों के अनुभव बताते हैं कि व्यतीत की सुधि नये सपने भी रचती है और उपलब्ध समय का आस्वाद भी समृद्ध करती है। जब ध्यान आता है कि किस बिन्दु से चलकर राह की कितनी विकट जटिलता से जूझते हम कहाँ पहुँचे हैं तो लोकयात्रा की थकान थोड़ी कम होती है, और तब हम अपने वर्तमान और भविष्य के प्रति काफ़ी हद तक आश्वस्त हो पाते हैं।
सन्तों की दुनिया का सत्य होगा कि अतीत-भविष्य को न देखकर वर्तमान पर ध्यान केन्द्रित करना सुख का रास्ता है। मगर आम आदमी इस अनुशासन को सहज ही स्वीकार नहीं कर पाता। और न तो रचनाकार अतीतजीवी कहे जाने के आतंक से उस कीर्तिशेष जगत् को बलात् भूल जाने का स्वाँग करता है, जिसने जगत् के अक्षर बाँचनेवाली संवेदनशील आँख दी है। जागरुक पाठक भी उन कृति पुरुषों के अन्तरंग जीवन के प्रच्छन्न-प्रकट रूप का सटीक परिचय पाने को सहज ही उत्सुक रहते हैं, जिनके साहित्य से उनका समीपी परिचय होता है। बाबू राय कृष्णदास, आचार्य शिवपूजन सहाय, श्री रामनाथ ‘सुमन’ और पाण्डेय बेचन शर्मा ‘उग्र’ का व्यक्तिपरक लेखन और परवर्ती काल में महादेवी वर्मा के संस्मरण, अज्ञेय की ‘स्मृतिलेखा’ तथा आचार्य जानकीवल्लभ शास्त्री की पुस्तक ‘हंसबलाका’ में संकलित व्यक्तिपरक निबन्ध हिन्दी संस्मरण-साहित्य के उत्कृष्ट उदाहण हैं जिनके माध्यम से उस काल के रचनाशील जगत् की तस्वीर उजागर हो जाती है बाद की पीढ़ी के पण्डितों-रचनाकारों ने मार्मिक संस्मरण लिखकर इस विधा को सम्पन्नतर किया। काशी-प्रवास काल पर केन्द्रित मेरे लेखों को पढ़कर श्री से. रा.यात्री, श्री कर्मेन्दु शिशिर और डॉ. अवधेश प्रधान ने अपने प्रेरक पत्र द्वारा संस्मरण-निबन्ध लिखने का आग्रह किया तो मैं कर्तव्य-सचेत हुआ कि जिनकी आत्मीय उपस्थिति मेरी संवेदना में उजास रचती रही है, उन स्मृतिशेष लोगों का तर्पण ज़रूरी दायित्व है।
और पुराने प्रसंगों को टाँगते समय जीवन का व्यतीत आस्वाद एक बार ताज़ा हो गया, और जम्हाई लेती साँझ यकायक हँसमुख लगने लगने लगी।
इस संकलन के निबन्ध जिन चरित्रों पर केन्द्रित हैं, उनकी भौतिक अनुपस्थिति में लिखे गये हैं। इसलिए अपने समय की संवेदना को विभिन्न बिन्दुओं के माध्यम से आँकते जो भी प्रसंग मेरे लेखन में आये हैं, उसके लिए मैं स्वयं को उत्तरदायी मानता हूँ विशेष कुछ दावा न कर विनम्रतापूर्वक इतना निवेदन करना जरूरी जान पड़ता है कि भरकस सजग रहा हूँ, ताकि मेरा एक भी शब्द तथ्य का धरातल न छोड़े। पुराने प्रसंग को टाँकते समय सुधि-शिल्पी का चेहरा हर चरण पर दिखाई पड़ता है; आरोपण का आग्रह नहीं, लेखक की लाचारी कदाचित् असहज नहीं लगेगी और सहृदय-क्षम्य होगी।
प्रसंगवश मन में कई प्रश्न जगे हैं-नयी पीढ़ी के प्रति शुभ-चिन्ता के आग्रह से, जिन्हें जस-का-तस प्रकट कर दिया है। मेरे प्रश्नों का उद्देश्य किसी की अवमानना क़तई नहीं है। इन्हें नये विमर्श-मंच के रचनात्मक आमन्त्रण के रूप में लिया जाय, शायद तभी लेखक के प्रति न्याय होगा। और प्रश्न अपेक्षित प्रभाव जगा सके तो उसे मैं अपने लेखक की उपलब्धि मानूँगा। उपलब्धि किसे काम्य नहीं होती। स्मृति का दायरा बड़ा है। और जब संस्मरण-निबन्ध लिखना शुरू किया तो अपने विद्या-परिवार के कई आत्मायजन की अनायास याद आयी। ज्येष्ठजन और अन्तरंग मित्रों की याद। पूरी ऊर्जा के साथ जो परिणय वय में भी सक्रिय हैं, ऐसे अनेक आत्मीय लोगों के बारे में भी निबन्ध लिखे। उन निबन्धों को दूसरे स्वतन्त्र संकलन में प्रस्तुत करना उचित जान पड़ा।
सक्रिय बने रहने के लिए बुढ़ौती सहारा खोजती है। मगर आज की भागाभागी वाली जीवनचर्या में साँस लेनेवाले के लिए किसी और के लिए अवकाश निकाल पाना प्रायः असम्भव हो गया है। अन्तर्वैयक्तिक रिश्ते की ढाही से आक्रान्त आज के कठकरेजी युग में सक्रिय सहयोग में आश्वस्त करते हैं कि संवेदनशीलता अभी, क्षीण रूप में ही सही, जीवित है। आयुष्मान रामनाथ के सहयोग से ही पुस्तक की प्रेस कॉपी तैयार हो सकी। सद्भाव और आशीर्वाद का यदि कुछ भी मूल्य है तो वह मूल्य चुकाने में भी मैंने कभी कोताही नहीं की है।
इस पुस्तक को प्रकाशित करने कि लिए मैं भारतीय ज्ञानपीठ का आभारी हूँ। प्रूफ संशोधन में मेरे प्रीतिभाजन श्रीराम तिवारी ने अपेक्षित सहयोग दिया।
सक्रियता सान्ध्य-वेला को हँसमुख बनाती है। जिस व्याज और जिनकी प्रेरणा से मेरी सक्रियता क़ायम है, सबके प्रति कृतज्ञ हूँ।
7-बी, हरिमोहन राय लेन
कोलकाता-700 015
25 अगस्त, 2001
साहित्य के मशहूर लण्ठ आचार्य माने जाते हैं- हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ लेखक।’’ स्पष्ट है कि अपने समय से शिकायत पहले भी उन तमाम लोगों को थी, जो मूल्यों के पक्षधर थे, साधना के पक्षधर, अगवाह राह के राही नहीं और जो व्यवस्था-प्रवीण लोगों के उन्नत हो रहे वर्चस्व को लक्ष्य कर निराला की तरह दुःखी थे। तथ्य है कि दूध से धुले लोगों की वह पीढ़ी नहीं थी, श्यामता का गहरा स्पर्श आदर्श के राग में जीने वाला समय भी ढो रहा था, अभिशाप के रूप में। श्री रामनाथ ‘सुमन’, पाण्डेय बेचन शर्मा ‘उग्र’ और राय कृष्णदास के संस्मरण इसी तथ्य की सम्पुष्टि करनेवाले साक्ष्य हैं। जो बड़ी बात थी उस पीढ़ी के साथ वह उनका सृजनशील जीवन था, जो समय की चुनौतियों को पीठ न दिखाकर अपनी जुझारू साधना से आनेवाले लोगों के लिए राह बना रहा था;
समय के लिए रोशनी रच रहा था।
यथार्थ के नाम पर कालिख-कलुष बटोरना–परोसना शिविर-विशेष द्वारा प्रगतिशील भूमिका मानी जा सकती है, पर हमें तलाश रहती है उस उज्ज्वल रोशनी की जो विचलित कर देनेवाले झंझावातों का मुक़ाबला करते खँडहरों में दबे दीये की बाती बनकर जल रही होती है, समय को तमस में हम विरासत के पन्नों को उलटते-पलटते हैं। राख के लिए नहीं, ऊष्मा के लिए हम साहित्य से जुड़ते हैं ताकि ठिठुरती-पथराती संवेदना टाँठ और गत्वर हो सके।
बुढ़ौती लोकयात्रा का ऐसा संवेदनशील पड़ाव है, जिसे स्पर्श करते ही व्यतीत की सुधि तीव्र हो जाती है। बूढ़ी साँझ सामान्यतः उदास होती है। और सुधि में सीझना बूढ़ों की नियति बन जाती है, यह उदास ही नहीं बन जाती है, यह अनुभवी बताते हैं। मगर साँझ-वेला में अकसर जागनेवाली सुधि केवल उदास ही नहीं बनाती, उस लोक से भी मन को जोड़ती है, जिसने हमारे जीवन-अनुशासन को रचा है और जागतिक अन्धड़ से पंजा लड़ाने की कला सिखायी है। अपने व्यतीत की पड़ताल करते उन परिदृश्यों, चेहरे-चरित्रों की बरबस याद आती है, जो हमारे सपने थे, अपने थे और जिनके अन्तरंग सान्निध्य में साँस लेते विकट प्रत्यूहों से टकरा-टकराकर हम अपनी ज़मीन तैयार करते रहे हैं।
अतीत-स्मृति का आस्वाद वर्तमान के स्वाद को हर समय फ़ीका नहीं करता, म्लान पड़ रही जीवन-प्रियता को रससिक्त कर पुनर्नवा भी करता है। और तब हम अपने सौभाग्य का साक्षात्कार कर साँझ की हँसमुख मुद्रा की सहज प्रेरणा से अवसाद की आँच में सीझने से स्वयं को बचा पाते हैं। सृजनशील ऊर्जा की रक्षा ही स्व की सुरक्षा की समुचित विधि है। कृती पुरुषों के अनुभव बताते हैं कि व्यतीत की सुधि नये सपने भी रचती है और उपलब्ध समय का आस्वाद भी समृद्ध करती है। जब ध्यान आता है कि किस बिन्दु से चलकर राह की कितनी विकट जटिलता से जूझते हम कहाँ पहुँचे हैं तो लोकयात्रा की थकान थोड़ी कम होती है, और तब हम अपने वर्तमान और भविष्य के प्रति काफ़ी हद तक आश्वस्त हो पाते हैं।
सन्तों की दुनिया का सत्य होगा कि अतीत-भविष्य को न देखकर वर्तमान पर ध्यान केन्द्रित करना सुख का रास्ता है। मगर आम आदमी इस अनुशासन को सहज ही स्वीकार नहीं कर पाता। और न तो रचनाकार अतीतजीवी कहे जाने के आतंक से उस कीर्तिशेष जगत् को बलात् भूल जाने का स्वाँग करता है, जिसने जगत् के अक्षर बाँचनेवाली संवेदनशील आँख दी है। जागरुक पाठक भी उन कृति पुरुषों के अन्तरंग जीवन के प्रच्छन्न-प्रकट रूप का सटीक परिचय पाने को सहज ही उत्सुक रहते हैं, जिनके साहित्य से उनका समीपी परिचय होता है। बाबू राय कृष्णदास, आचार्य शिवपूजन सहाय, श्री रामनाथ ‘सुमन’ और पाण्डेय बेचन शर्मा ‘उग्र’ का व्यक्तिपरक लेखन और परवर्ती काल में महादेवी वर्मा के संस्मरण, अज्ञेय की ‘स्मृतिलेखा’ तथा आचार्य जानकीवल्लभ शास्त्री की पुस्तक ‘हंसबलाका’ में संकलित व्यक्तिपरक निबन्ध हिन्दी संस्मरण-साहित्य के उत्कृष्ट उदाहण हैं जिनके माध्यम से उस काल के रचनाशील जगत् की तस्वीर उजागर हो जाती है बाद की पीढ़ी के पण्डितों-रचनाकारों ने मार्मिक संस्मरण लिखकर इस विधा को सम्पन्नतर किया। काशी-प्रवास काल पर केन्द्रित मेरे लेखों को पढ़कर श्री से. रा.यात्री, श्री कर्मेन्दु शिशिर और डॉ. अवधेश प्रधान ने अपने प्रेरक पत्र द्वारा संस्मरण-निबन्ध लिखने का आग्रह किया तो मैं कर्तव्य-सचेत हुआ कि जिनकी आत्मीय उपस्थिति मेरी संवेदना में उजास रचती रही है, उन स्मृतिशेष लोगों का तर्पण ज़रूरी दायित्व है।
और पुराने प्रसंगों को टाँगते समय जीवन का व्यतीत आस्वाद एक बार ताज़ा हो गया, और जम्हाई लेती साँझ यकायक हँसमुख लगने लगने लगी।
इस संकलन के निबन्ध जिन चरित्रों पर केन्द्रित हैं, उनकी भौतिक अनुपस्थिति में लिखे गये हैं। इसलिए अपने समय की संवेदना को विभिन्न बिन्दुओं के माध्यम से आँकते जो भी प्रसंग मेरे लेखन में आये हैं, उसके लिए मैं स्वयं को उत्तरदायी मानता हूँ विशेष कुछ दावा न कर विनम्रतापूर्वक इतना निवेदन करना जरूरी जान पड़ता है कि भरकस सजग रहा हूँ, ताकि मेरा एक भी शब्द तथ्य का धरातल न छोड़े। पुराने प्रसंग को टाँकते समय सुधि-शिल्पी का चेहरा हर चरण पर दिखाई पड़ता है; आरोपण का आग्रह नहीं, लेखक की लाचारी कदाचित् असहज नहीं लगेगी और सहृदय-क्षम्य होगी।
प्रसंगवश मन में कई प्रश्न जगे हैं-नयी पीढ़ी के प्रति शुभ-चिन्ता के आग्रह से, जिन्हें जस-का-तस प्रकट कर दिया है। मेरे प्रश्नों का उद्देश्य किसी की अवमानना क़तई नहीं है। इन्हें नये विमर्श-मंच के रचनात्मक आमन्त्रण के रूप में लिया जाय, शायद तभी लेखक के प्रति न्याय होगा। और प्रश्न अपेक्षित प्रभाव जगा सके तो उसे मैं अपने लेखक की उपलब्धि मानूँगा। उपलब्धि किसे काम्य नहीं होती। स्मृति का दायरा बड़ा है। और जब संस्मरण-निबन्ध लिखना शुरू किया तो अपने विद्या-परिवार के कई आत्मायजन की अनायास याद आयी। ज्येष्ठजन और अन्तरंग मित्रों की याद। पूरी ऊर्जा के साथ जो परिणय वय में भी सक्रिय हैं, ऐसे अनेक आत्मीय लोगों के बारे में भी निबन्ध लिखे। उन निबन्धों को दूसरे स्वतन्त्र संकलन में प्रस्तुत करना उचित जान पड़ा।
सक्रिय बने रहने के लिए बुढ़ौती सहारा खोजती है। मगर आज की भागाभागी वाली जीवनचर्या में साँस लेनेवाले के लिए किसी और के लिए अवकाश निकाल पाना प्रायः असम्भव हो गया है। अन्तर्वैयक्तिक रिश्ते की ढाही से आक्रान्त आज के कठकरेजी युग में सक्रिय सहयोग में आश्वस्त करते हैं कि संवेदनशीलता अभी, क्षीण रूप में ही सही, जीवित है। आयुष्मान रामनाथ के सहयोग से ही पुस्तक की प्रेस कॉपी तैयार हो सकी। सद्भाव और आशीर्वाद का यदि कुछ भी मूल्य है तो वह मूल्य चुकाने में भी मैंने कभी कोताही नहीं की है।
इस पुस्तक को प्रकाशित करने कि लिए मैं भारतीय ज्ञानपीठ का आभारी हूँ। प्रूफ संशोधन में मेरे प्रीतिभाजन श्रीराम तिवारी ने अपेक्षित सहयोग दिया।
सक्रियता सान्ध्य-वेला को हँसमुख बनाती है। जिस व्याज और जिनकी प्रेरणा से मेरी सक्रियता क़ायम है, सबके प्रति कृतज्ञ हूँ।
7-बी, हरिमोहन राय लेन
कोलकाता-700 015
25 अगस्त, 2001
-कृष्णबिहारी मिश्र
काशी के अन्तरंग रिशते को
याद करते हुए
मेरे रक्त में ही काशी के प्रति आकर्षण था। प्रपितामह-प्रपितामही और पितामह-पितामही ने जीवन के उपसंहार काल में ‘काशी-वास’ करते ‘मुक्ति क्षेत्र’ में ‘गंगा-लाभ’ किया था। मातृहीना इकलौती देहाती बेटी का विवाह बाबा ने किसी बड़ी साध के आग्रह से काशी में किया था और भतीजे को छठी कक्षा में ही गाँव से ले जाकर काशी के प्रसिद्ध विद्यालय जयनारायण स्कूल में भरती करा दिया था। चाचा हिन्दू विश्वविद्यालय के स्नातक बनकर गाँव लौटे थे और ऊँची शिक्षा का सारी सुविधा छोड़कर मैं कलकत्ता से दूर काशी पहुँच गया था, ऊँची शिक्षा की महत्त्वकांक्षा से।
बी.ए. प्रथम वर्ष में ही मातृ-वियोग ने मेरी साध पर वज्रघात किया था। उच्चाटन इतना गहरा था कि पढ़ाई में मन रम नहीं रहा था। काशी से पगहा तुड़ाकर कलकत्ता भागने को मन हर वक़्त व्याकुल रहता था। तभी शिवप्रसाद सिंह की आत्मीय संगति मिल गयी। उचटे मन को एक सहारा। उच्चाटन गिरफ़्त से पूरी तरह मन उबरा तो नहीं था, पर जीवनप्रियता पुनर्नवा हो चली थी। शोधकार्य करते शिवप्रसाद सिंह कुछ कक्षाओं में पढ़ाते भी थे। मेरी एक कक्षा में भी।
पर उनसे मेरा नाता शुरू से ही बड़े-छोटे भाई का था, अध्यापक-विद्यार्थी का नहीं। और वह बन्धु-भाव प्रगाढ़तर होता गया। वे तब गुर्टू हॉस्टल के 13 नं. कमरे में रहते थे, जहाँ रामदरश मिश्र, रवीन्द्र भ्रमर, विद्यासागर नौटियाल, केदारनाथ सिंह और विश्वनाथ त्रिपाठी रहते थे। इनके सर्जनशील भविष्य के प्रति ज्येष्ठजन आश्वस्त थे। गुर्टू हॉस्टल में अज्ञेय, नागार्जुन, जानकीवल्लभ शास्त्री, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन शास्त्री जैसे प्रतिष्ठित पांक्तेयजन प्रायः जाया करते थे। एक उदीयमान सम्भावना लोगों को बरबस खींचती थी। तब हिन्दू विश्वविद्यालय कृति अध्यापकों के समृद्ध था। प्रायः हर विभाग राष्ट्रीय प्रतिष्ठा-प्राप्त आचार्यों से सम्पन्न था। और उस वातावरण में मुझे भी रस मिलने लगा, जो मेरे उच्चाटन का सटीक उपचार था। साध को सही पटरी मिल गई थी। और अपनी सही ज़मीन पर धीरे-धीरे क्रियाशील हो चला था। डॉ. गणेश प्रसाद उनियाल और डॉ. विजय शंकर मल्ल की उच्छल वत्सलता मेरे लिए प्रेरक प्रोत्साहन था।
तुलसीदास की कुटिया के पिछवाड़े लोलार्क कुण्ड पर खड़े पीपल के पेड़ से सटे मकान में रहता था। मेरे मकान से सटे मकान में नामवर सिंह रहते थे। उनके ठीक सामने ही पं. शान्तिप्रिय द्विवेदी की सूनी कुटिया थी। शोधकार्य करते हुए नामवरजी विश्वविद्यालय में कक्षा भी लेते थे। उनकी प्रतिभा-योग्यता का क़ायल होते हुए भी मैंने उनकी मुद्रा में कभी आत्मीय आमन्त्रण लक्ष्य नहीं किया। शिष्टाचार में मेरी ओर से कभी चूक नहीं हुई। और उन्होंने मुझे अपने घर केवल एक बार अधिकारपूर्वक अपनी सेवा में आमन्त्रित किया था, जब अपने शोध-प्रबन्ध के रूपायन को अन्तिम स्पर्श दे रहे थे। नामवरजी जैसे विलक्षण व्यक्ति के लिए यह समझना कठिन नहीं था कि मेरी राशि शिवप्रसाद सिंह से मिलती थी। और नामवर सिंह की राह ज़रा अलग थी। गुर्टू हॉस्टल से अस्सी घाट तक सन्ध्याटन हमारी नित्य की चर्या थी। पं. शान्तिप्रिय द्विवेदी कण-कण से चिढ़नेवाले व्यक्ति थे-मुहल्ले में किसी से उनका आत्मीय सम्बन्ध नहीं था। मेरे प्रति किंचित् कृपालु थे। जब-तब मेरे यहाँ आ जाते थे। बड़े ज़ोर से साँकल बजाते थे। मैं उन्हें आदरपूर्वक ऊपर ले जाता था।
उन्होंने बताया था, उनकी बड़ी बहन इसी घर में रहती थीं। बहन, जो माँ प्रतिम थीं, की स्मृति उन्हें अकसर मेरे यहाँ खींच लाती थी, और भाव-पोषण से उनकी मुरझायी ज़िन्दगी को थोड़ा सहारा मिलता था। काफ़ी देर तक बैठे बतियाते रहते थे मगर उनसे बात करना बड़ा कठिन था। एक तो बहुत ऊँचा सुनते थे, दूसरे हर व्यक्ति के प्रति उनके मन में तीखी शिकायत थी। मुझे स्मरण है, अपने शहर के दो उदीयमान लेखकों के बारे में उन्होंने एक दिन बेहद खीझते हुए मुझसे कहा था- ‘‘नामवर सिंह ने मेरा सामाजिक बहिष्कार किया है। होली मिलन पर मैं उनके यहाँ जाता हूँ, वे मेरे यहाँ नहीं आते, जबकि मेरे दरवाज़े के सामने रहते हैं और शिवप्रसाद सिंह मेरे बारे में कभी कुछ लिखते नहीं। उन्होंने मेरा साहित्यिक बहिष्कार किया है।’’ उनके कण्ठ से मैंने आचार्य केशवप्रसाद मिश्र को छोड़कर किसी की प्रशंसा नहीं सुनी। अकसर कहते थे-‘‘केशवजी जीवित होते तो अब तक मुझे डी.लिट्. का सम्मान मिल गया होता।’’ उन्हीं दिनों ‘अवन्तिका’ में उनके बारे में नामवर सिंह का लेख छपा था। उन्हीं दिनों उनका आत्मपरक उपन्यास ‘दिगम्बर’ छपा था। और आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी को भेंट करते उन्हें मैंने सुना था-‘‘आप अपनी पुस्तक मुझे नहीं देते, मगर मैं अपनी हर पुस्तक आप तक पहुँचाना चाहता हूँ।’’ वाजपेयी जी ने मुस्कुराते हुए कहा था- ‘‘मैं भी अपनी पुस्तक आपको भेजूँगा ।’’ पता नहीं, शान्तिप्रिय जी ने उनकी बात सुनी या नहीं, अपना आग्रह प्रकट किया-‘‘गोदान से आगे की रचना है, पढ़िएगा।’’ और मुस्कराते हुए वाजपेयीजी मंच की ओर बढ़ गये थे।
जीवनप्रिय पं. शान्तिप्रिय द्विवेदी एक त्रासद सन्नाटे में जीने को अभिशप्त थे। निपट अकेले। न अपना घर, न अपनी गृहस्थी। उनका अन्तरंग मित्र कौन था, पता नहीं। उनके यहाँ कभी किसी को आते-जाते नहीं देखता था। शाम को वे अकेले कभी गोदौलिया, कभी अस्सी चौमुहानी पर टहलते दिखाई पड़ते थे धोबी, रिक्शेवाले और दूधवाले से लड़ते-झगड़ते अक्सर उन्हें देखा था। और ज्येष्ठ विद्या-साधक के पक्ष में कई बार मुझे ख़डा होना पड़ा था।
कई बार अपने अनुकूल मेरा आचरण न देखकर उन्होंने विक्षोभक मुद्रा में डाटा भी था। एक दिन गदौलिया की भीड़-भरी पटरी पर पीछे से उन्होंने मुझे आवाज़ दी। मुड़कर मैंने प्रणाम किया तो बोले कि ‘‘युग का विपर्यय यह है कि ब्राह्मण ठाकुर के पीछे-पीछे घूम रहा है।’’ अपनी सामान्य चर्चा के मुताबिक मैं शिवप्रसाद सिंह के साथ शाम को घूमने निकला था। भीड़ में वे आगे थे, मैं पीछे। मैंने नम्रतापूर्वक निवेदन किया-‘‘ये ब्राह्मण हैं, पण्डित जी।’’ नहीं मैं जानता हूँ, ये ठाकुर हैं, शिवप्रसाद सिंह है।’’ और चमककर वे दूसरी ओर मुड़ गये। एक बार उन्होंने अपनी अंतरंग पीड़ा प्रकट की थी-‘‘होटल और वेश्यालय मनुष्य को परितृप्ति नहीं देता, गृहस्थी के आस्वाद से ही मनुष्य तुष्ट होता है। पं. शान्तिप्रिय द्विवेदी ने मेरे घर शरबत पीते मुझसे कहा था-‘‘कलकत्ता से आपका रिश्ता है। लम्बी छुट्टी में जब जाइए, बंगीय रुचिवाली कोई लड़की देखिए !’’ पचासा पार करने के बाद भी वे अपने लिए लड़की तलाश रहे थे, जो मेरे लिए चौकानेवाली बात थी। उनकी कुटिया में मैंने एक रूपवती महिला का चित्र देखा था।
परिचय पूछने पर उन्होंने सिर्फ़ इतना ही कहा था-‘‘आँख की मुद्रा कितनी मोहक-मुखर है। केश राशि की शोभा देखिए !’’ जब चलने लगा तो उन्होंने आदेश दिया, इस अन्दाज़ से जैसे मुझे विद्या के ऊँचे सोपान की सीढ़ी दिखा रहे हों।-‘‘दिगम्बर ख़रीदकर पढ़िए। ऐसा उपन्यास हिन्दी में लिखा नहीं गया।’’ और मैंने वह लघु उपन्यास ख़रीद लिया था आत्ममुग्ध लेखक का दावा जितना बड़ा था, उस कोटि की सर्जनशीलता ‘दिगम्बर’ में मुझे नहीं दिखाई पड़ी। आत्मरति की भावुक अभिव्यक्ति के सिवा मुझे उसमें कुछ नहीं मिला। अतृप्त दमित वासना की एक सतही अभिव्यक्ति। बेशक पं. शान्तिप्रियजी अपनी पीढ़ी के नामी समीक्षक थे। उनकी कीर्ति छायावादी काव्य, मुख्यतः पन्तजी की कविता, के सहृदय समीक्षक के रूप में थी। विशारद की परीक्षा देने की जब तैयारी कर रहा था, उनकी ‘संचारिणी’ पढ़ी थी, और उनकी व्यंजक उदभावनाओं का मेरे मन पर असर था। उन्हें अपेक्षित सम्मान देना तो मेरे लिए सहज था, पर उनकी जटिल अपेक्षा पूरी करना बड़ा विकट था पचासा पार करने के बाद भी वे गृहस्थी बसाने के लिए व्याकुल थे। पर बंगीय रुचि की हिन्दीभाषी युवती उनके लिए खोज पाना मेरे जैसे आदमी के लिए असम्भव था। और यह भी सम्भव नहीं था। कि मैं ‘दिगम्बर’ को ‘गोदान’ से बड़ी औपन्यासिक कृति मान लूँ। सो मेरे प्रति उनका मोहभंग होने लगा।
मगर उस मुहल्ले में मेरे अलावा शायद कोई और था ही नहीं, जिससे वे अपने निजी प्रयोजन की बातें करते। लोलार्क कुण्ड छोड़कर जब मैं जानकी घाट पर बाबू अशर्फी सिंह के मकान में रहने लगा। शान्तिप्रियजी उच्चाटन का आवेग बढ़ने पर यदा-कदा वहाँ भी पधारते थे। एक दिन बड़े गुस्से में पहुँचे। नाराज़गी कहीं और थी और बरस मुझपर रहे थे-‘‘हिन्दी में एम.ए. पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आचार्य केशव प्रसाद जी को जानते हैं ? आपको पता है केशवजी मेरी कितनी इज़्ज़त करते थे ? वे जीवित होते तो मुझे डी.लिट्. की उपाधि मिल गई होती। हजारी प्रासाद द्विवेदी की तरह वे बहरे नहीं थे बनारस में एक द्विवेदी अन्धा है, दूसरा द्विवेदी बहरा है। एक किसी की किताब पढ़ता नहीं, दूसरा किसी की बात सुनता नहीं। और भरनेवाले चाटुकार कुछ-का-कुछ कान में भर देते हैं आप यथार्थ का बोध कराइये। अपने गुरु से कहिए, हिन्दी विभाग में व्याख्यान करावें।’’ अनेक प्रकार की अतृप्त भूख ने शान्तप्रिय जी को कर्कश बना दिया था। उन्हें देखने और बतकही करने पर लगता था, रस का एक क़तरा भी उसके व्यक्तित्व में शेष नहीं है। स्वयं बधिर होते हुए मेरे गुरु पं. हजारीप्रसाद द्विवेदी को बहरा कह रहे थे। और गुरु-प्रतिम मेरे पूज्य पं. रामअवध द्विवेदी के दुर्भाग्य पर तीखा कटाक्ष कर रहे थे। मैंने अपने भीतर क्रोध की तेज़ आँच महसूस की थी, पर शिष्टाचार्य का दबाव था कि उनका प्रलाप चुपचाप सुनता रहा। मगर मन की तीखी प्रतिक्रिया चेहरे पर शायद मुखर हो गई थी, जिसे शायद द्विवेदी जी ने लक्ष्य भी लिया था। श्रीहीन गलित अनुनय की मुद्रा में उन्होंने आग्रह किया-‘‘आपसे ही सम्भव होगा।
हजारीप्रसाद आपकी बात सुनेंगे, मेरा भाषण करा दीजिए, हिन्दी विभाग में।’ लेखक के स्वाभिमान के विपरीत थी वह मुद्रा। ऊँची आवाज़ में मैंने उन्हें टोका- ‘‘पण्डितजी, हिन्दी विभाग के लिए यह गौरव की बात होगी कि आप वहाँ व्याख्यान दें। आपके प्रति यह विभागाध्यक्ष का अनुग्रह नहीं होगा।’’ प्रीत होकर उन्होंने कहा, ‘‘आप ही जैसे संस्कारी युवक पर समाज टिका हुआ है।’’ और चलते बने मगर उनकी बतकही ने मुझे भीतर से घायल कर दिया था। राह-घाट में कहीं दूर दिखाई पड़ते शान्तिप्रियजी तो बग़ल की राह पकड़कर उनकी संगति से बचने की कोशिश करने लगा था। एक दिन अस्सी चौमुनाही पर उन्होंने मुझे पकड़ लिया और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे-‘‘ द्विवेदीजी से बात कीजिए। छुट्टियाँ करीब हैं, फिर बात बिगड़ जाएगी ।’’
उनकी मुद्रा ने मेरे क्षोभ को फिर उत्तेजित किया। पर चुप लगा गया। अन्ततः उनकी साध हिन्दी विभागाध्यक्ष पं. हजारीप्रसाद द्विवेदी तक पहुँचाने की लाचारी थी। सुनते ही पण्डितजी ने अपनी सहज शैली में ज़ोर का ठहाका लगाया। फिर उनका आदेश था-‘‘डॉक्टर श्रीकृष्ण लालजी से बात करके समय तय कर लो और एक दिन शान्तिप्रियजी को विभाग में ले आओ।’’ लोलार्क कुण्ड से उन्हें हिन्दी विभाग में ले गया। छात्रों-अध्यापकों की संख्या बहुत कम थी। छात्राएँ और भी कम, नहीं के बराबर। कम उपस्थिति वक्ता को चिढ़ाने के लिए बहुत थी तथापि उन्होंने अपने ढंग से व्याख्यान दिया। पण्डित जी ने उनकी प्रशंसा में बहुत-कुछ-कहा, शिष्टाचारवश, अपने सहज कौशल के अनुरूप। पर द्विवेदी जी को बधिर माननेवाले पं. शान्तिप्रियजी ने पता नहीं कितना-कुछ सुना और उससे उनके मन का कितना समाधन हुआ। दो दिन बाद उनके गहरे असन्तोष का पता चला। मिलते ही कहने लगे-‘‘.....ने कक्षा से लड़कियों को अपने कूट कौशल से भगा दिया था। आप बहुत सीधे हैं। चालाकी समझ नहीं पाते। एक दूसरा कार्यक्रम कराइए, जिसमें छात्राएँ उपस्थित रहें। कार्यक्रम तय करके मुझे खबर दीजिए।’’
बड़ा संकट था, पण्डितजी के सामने फिर यह प्रसंग उठाना नहीं चाहिए था। शान्तिप्रियजी के हठ का क्या उपचार किया जाए ! पण्डित जी के व्यंजक ठहाका कई बार जटिल प्रसंग का समाधन कर देता था। उन्होंने सहज भाव से एक दिन पूछा, ‘‘कहो, पं. शान्तिप्रियजी का क्या हाल है ? अब तो तुष्ट हैं न ?’’ मेरा असमंजस टूट गया । मैंने उनकी शिकायत और आग्रह पण्डितजी के सामने जस-का-तस रख दिया। पण्डित जी ने बड़े ज़ोर का ठहाका लगाया !
काशी की प्रसिद्ध विद्या-विभूति पं. चन्द्रबली पाण्डेय यद्यपि विश्वविद्यालय सेवा से जुड़े थे, पर विश्वविद्यालय परिसर में ही अपने मित्र मौलवी महेश प्रसाद के साथ रहते थे। बाद में वे डॉ. ज्ञानवती त्रिवेदी के बँगले पर आ गये थे। पं. शान्तिप्रियजी और पं. चन्द्रबली पाण्डेय आजमगढ़ के विद्या-रत्न थे, और आजमगढ़ के राहुल सांकृत्यायन को अपने जनपत के पं. चन्द्रबली पाण्डेय, पं. लक्ष्मीनाराण मिश्र और पं. शान्तिप्रिय द्विवेदी की विद्या-साधना का सहज गर्व था। ‘अपनी जीवन-यात्रा में राहुलजी ने अपनी भावना प्रकट की है। हैदराबाद हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सन्दर्भ में, जिसके अध्यक्ष पं. चन्द्रबली पाण्डेय थे और सहित्य परिषद् के अध्यक्ष पं. लक्ष्मीनारायण मिश्र थे। मैंने शान्तिप्रियजी के प्रति राहुलजी की आत्मीयता देखी है।
बी.ए. प्रथम वर्ष में ही मातृ-वियोग ने मेरी साध पर वज्रघात किया था। उच्चाटन इतना गहरा था कि पढ़ाई में मन रम नहीं रहा था। काशी से पगहा तुड़ाकर कलकत्ता भागने को मन हर वक़्त व्याकुल रहता था। तभी शिवप्रसाद सिंह की आत्मीय संगति मिल गयी। उचटे मन को एक सहारा। उच्चाटन गिरफ़्त से पूरी तरह मन उबरा तो नहीं था, पर जीवनप्रियता पुनर्नवा हो चली थी। शोधकार्य करते शिवप्रसाद सिंह कुछ कक्षाओं में पढ़ाते भी थे। मेरी एक कक्षा में भी।
पर उनसे मेरा नाता शुरू से ही बड़े-छोटे भाई का था, अध्यापक-विद्यार्थी का नहीं। और वह बन्धु-भाव प्रगाढ़तर होता गया। वे तब गुर्टू हॉस्टल के 13 नं. कमरे में रहते थे, जहाँ रामदरश मिश्र, रवीन्द्र भ्रमर, विद्यासागर नौटियाल, केदारनाथ सिंह और विश्वनाथ त्रिपाठी रहते थे। इनके सर्जनशील भविष्य के प्रति ज्येष्ठजन आश्वस्त थे। गुर्टू हॉस्टल में अज्ञेय, नागार्जुन, जानकीवल्लभ शास्त्री, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन शास्त्री जैसे प्रतिष्ठित पांक्तेयजन प्रायः जाया करते थे। एक उदीयमान सम्भावना लोगों को बरबस खींचती थी। तब हिन्दू विश्वविद्यालय कृति अध्यापकों के समृद्ध था। प्रायः हर विभाग राष्ट्रीय प्रतिष्ठा-प्राप्त आचार्यों से सम्पन्न था। और उस वातावरण में मुझे भी रस मिलने लगा, जो मेरे उच्चाटन का सटीक उपचार था। साध को सही पटरी मिल गई थी। और अपनी सही ज़मीन पर धीरे-धीरे क्रियाशील हो चला था। डॉ. गणेश प्रसाद उनियाल और डॉ. विजय शंकर मल्ल की उच्छल वत्सलता मेरे लिए प्रेरक प्रोत्साहन था।
तुलसीदास की कुटिया के पिछवाड़े लोलार्क कुण्ड पर खड़े पीपल के पेड़ से सटे मकान में रहता था। मेरे मकान से सटे मकान में नामवर सिंह रहते थे। उनके ठीक सामने ही पं. शान्तिप्रिय द्विवेदी की सूनी कुटिया थी। शोधकार्य करते हुए नामवरजी विश्वविद्यालय में कक्षा भी लेते थे। उनकी प्रतिभा-योग्यता का क़ायल होते हुए भी मैंने उनकी मुद्रा में कभी आत्मीय आमन्त्रण लक्ष्य नहीं किया। शिष्टाचार में मेरी ओर से कभी चूक नहीं हुई। और उन्होंने मुझे अपने घर केवल एक बार अधिकारपूर्वक अपनी सेवा में आमन्त्रित किया था, जब अपने शोध-प्रबन्ध के रूपायन को अन्तिम स्पर्श दे रहे थे। नामवरजी जैसे विलक्षण व्यक्ति के लिए यह समझना कठिन नहीं था कि मेरी राशि शिवप्रसाद सिंह से मिलती थी। और नामवर सिंह की राह ज़रा अलग थी। गुर्टू हॉस्टल से अस्सी घाट तक सन्ध्याटन हमारी नित्य की चर्या थी। पं. शान्तिप्रिय द्विवेदी कण-कण से चिढ़नेवाले व्यक्ति थे-मुहल्ले में किसी से उनका आत्मीय सम्बन्ध नहीं था। मेरे प्रति किंचित् कृपालु थे। जब-तब मेरे यहाँ आ जाते थे। बड़े ज़ोर से साँकल बजाते थे। मैं उन्हें आदरपूर्वक ऊपर ले जाता था।
उन्होंने बताया था, उनकी बड़ी बहन इसी घर में रहती थीं। बहन, जो माँ प्रतिम थीं, की स्मृति उन्हें अकसर मेरे यहाँ खींच लाती थी, और भाव-पोषण से उनकी मुरझायी ज़िन्दगी को थोड़ा सहारा मिलता था। काफ़ी देर तक बैठे बतियाते रहते थे मगर उनसे बात करना बड़ा कठिन था। एक तो बहुत ऊँचा सुनते थे, दूसरे हर व्यक्ति के प्रति उनके मन में तीखी शिकायत थी। मुझे स्मरण है, अपने शहर के दो उदीयमान लेखकों के बारे में उन्होंने एक दिन बेहद खीझते हुए मुझसे कहा था- ‘‘नामवर सिंह ने मेरा सामाजिक बहिष्कार किया है। होली मिलन पर मैं उनके यहाँ जाता हूँ, वे मेरे यहाँ नहीं आते, जबकि मेरे दरवाज़े के सामने रहते हैं और शिवप्रसाद सिंह मेरे बारे में कभी कुछ लिखते नहीं। उन्होंने मेरा साहित्यिक बहिष्कार किया है।’’ उनके कण्ठ से मैंने आचार्य केशवप्रसाद मिश्र को छोड़कर किसी की प्रशंसा नहीं सुनी। अकसर कहते थे-‘‘केशवजी जीवित होते तो अब तक मुझे डी.लिट्. का सम्मान मिल गया होता।’’ उन्हीं दिनों ‘अवन्तिका’ में उनके बारे में नामवर सिंह का लेख छपा था। उन्हीं दिनों उनका आत्मपरक उपन्यास ‘दिगम्बर’ छपा था। और आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी को भेंट करते उन्हें मैंने सुना था-‘‘आप अपनी पुस्तक मुझे नहीं देते, मगर मैं अपनी हर पुस्तक आप तक पहुँचाना चाहता हूँ।’’ वाजपेयी जी ने मुस्कुराते हुए कहा था- ‘‘मैं भी अपनी पुस्तक आपको भेजूँगा ।’’ पता नहीं, शान्तिप्रिय जी ने उनकी बात सुनी या नहीं, अपना आग्रह प्रकट किया-‘‘गोदान से आगे की रचना है, पढ़िएगा।’’ और मुस्कराते हुए वाजपेयीजी मंच की ओर बढ़ गये थे।
जीवनप्रिय पं. शान्तिप्रिय द्विवेदी एक त्रासद सन्नाटे में जीने को अभिशप्त थे। निपट अकेले। न अपना घर, न अपनी गृहस्थी। उनका अन्तरंग मित्र कौन था, पता नहीं। उनके यहाँ कभी किसी को आते-जाते नहीं देखता था। शाम को वे अकेले कभी गोदौलिया, कभी अस्सी चौमुहानी पर टहलते दिखाई पड़ते थे धोबी, रिक्शेवाले और दूधवाले से लड़ते-झगड़ते अक्सर उन्हें देखा था। और ज्येष्ठ विद्या-साधक के पक्ष में कई बार मुझे ख़डा होना पड़ा था।
कई बार अपने अनुकूल मेरा आचरण न देखकर उन्होंने विक्षोभक मुद्रा में डाटा भी था। एक दिन गदौलिया की भीड़-भरी पटरी पर पीछे से उन्होंने मुझे आवाज़ दी। मुड़कर मैंने प्रणाम किया तो बोले कि ‘‘युग का विपर्यय यह है कि ब्राह्मण ठाकुर के पीछे-पीछे घूम रहा है।’’ अपनी सामान्य चर्चा के मुताबिक मैं शिवप्रसाद सिंह के साथ शाम को घूमने निकला था। भीड़ में वे आगे थे, मैं पीछे। मैंने नम्रतापूर्वक निवेदन किया-‘‘ये ब्राह्मण हैं, पण्डित जी।’’ नहीं मैं जानता हूँ, ये ठाकुर हैं, शिवप्रसाद सिंह है।’’ और चमककर वे दूसरी ओर मुड़ गये। एक बार उन्होंने अपनी अंतरंग पीड़ा प्रकट की थी-‘‘होटल और वेश्यालय मनुष्य को परितृप्ति नहीं देता, गृहस्थी के आस्वाद से ही मनुष्य तुष्ट होता है। पं. शान्तिप्रिय द्विवेदी ने मेरे घर शरबत पीते मुझसे कहा था-‘‘कलकत्ता से आपका रिश्ता है। लम्बी छुट्टी में जब जाइए, बंगीय रुचिवाली कोई लड़की देखिए !’’ पचासा पार करने के बाद भी वे अपने लिए लड़की तलाश रहे थे, जो मेरे लिए चौकानेवाली बात थी। उनकी कुटिया में मैंने एक रूपवती महिला का चित्र देखा था।
परिचय पूछने पर उन्होंने सिर्फ़ इतना ही कहा था-‘‘आँख की मुद्रा कितनी मोहक-मुखर है। केश राशि की शोभा देखिए !’’ जब चलने लगा तो उन्होंने आदेश दिया, इस अन्दाज़ से जैसे मुझे विद्या के ऊँचे सोपान की सीढ़ी दिखा रहे हों।-‘‘दिगम्बर ख़रीदकर पढ़िए। ऐसा उपन्यास हिन्दी में लिखा नहीं गया।’’ और मैंने वह लघु उपन्यास ख़रीद लिया था आत्ममुग्ध लेखक का दावा जितना बड़ा था, उस कोटि की सर्जनशीलता ‘दिगम्बर’ में मुझे नहीं दिखाई पड़ी। आत्मरति की भावुक अभिव्यक्ति के सिवा मुझे उसमें कुछ नहीं मिला। अतृप्त दमित वासना की एक सतही अभिव्यक्ति। बेशक पं. शान्तिप्रियजी अपनी पीढ़ी के नामी समीक्षक थे। उनकी कीर्ति छायावादी काव्य, मुख्यतः पन्तजी की कविता, के सहृदय समीक्षक के रूप में थी। विशारद की परीक्षा देने की जब तैयारी कर रहा था, उनकी ‘संचारिणी’ पढ़ी थी, और उनकी व्यंजक उदभावनाओं का मेरे मन पर असर था। उन्हें अपेक्षित सम्मान देना तो मेरे लिए सहज था, पर उनकी जटिल अपेक्षा पूरी करना बड़ा विकट था पचासा पार करने के बाद भी वे गृहस्थी बसाने के लिए व्याकुल थे। पर बंगीय रुचि की हिन्दीभाषी युवती उनके लिए खोज पाना मेरे जैसे आदमी के लिए असम्भव था। और यह भी सम्भव नहीं था। कि मैं ‘दिगम्बर’ को ‘गोदान’ से बड़ी औपन्यासिक कृति मान लूँ। सो मेरे प्रति उनका मोहभंग होने लगा।
मगर उस मुहल्ले में मेरे अलावा शायद कोई और था ही नहीं, जिससे वे अपने निजी प्रयोजन की बातें करते। लोलार्क कुण्ड छोड़कर जब मैं जानकी घाट पर बाबू अशर्फी सिंह के मकान में रहने लगा। शान्तिप्रियजी उच्चाटन का आवेग बढ़ने पर यदा-कदा वहाँ भी पधारते थे। एक दिन बड़े गुस्से में पहुँचे। नाराज़गी कहीं और थी और बरस मुझपर रहे थे-‘‘हिन्दी में एम.ए. पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आचार्य केशव प्रसाद जी को जानते हैं ? आपको पता है केशवजी मेरी कितनी इज़्ज़त करते थे ? वे जीवित होते तो मुझे डी.लिट्. की उपाधि मिल गई होती। हजारी प्रासाद द्विवेदी की तरह वे बहरे नहीं थे बनारस में एक द्विवेदी अन्धा है, दूसरा द्विवेदी बहरा है। एक किसी की किताब पढ़ता नहीं, दूसरा किसी की बात सुनता नहीं। और भरनेवाले चाटुकार कुछ-का-कुछ कान में भर देते हैं आप यथार्थ का बोध कराइये। अपने गुरु से कहिए, हिन्दी विभाग में व्याख्यान करावें।’’ अनेक प्रकार की अतृप्त भूख ने शान्तप्रिय जी को कर्कश बना दिया था। उन्हें देखने और बतकही करने पर लगता था, रस का एक क़तरा भी उसके व्यक्तित्व में शेष नहीं है। स्वयं बधिर होते हुए मेरे गुरु पं. हजारीप्रसाद द्विवेदी को बहरा कह रहे थे। और गुरु-प्रतिम मेरे पूज्य पं. रामअवध द्विवेदी के दुर्भाग्य पर तीखा कटाक्ष कर रहे थे। मैंने अपने भीतर क्रोध की तेज़ आँच महसूस की थी, पर शिष्टाचार्य का दबाव था कि उनका प्रलाप चुपचाप सुनता रहा। मगर मन की तीखी प्रतिक्रिया चेहरे पर शायद मुखर हो गई थी, जिसे शायद द्विवेदी जी ने लक्ष्य भी लिया था। श्रीहीन गलित अनुनय की मुद्रा में उन्होंने आग्रह किया-‘‘आपसे ही सम्भव होगा।
हजारीप्रसाद आपकी बात सुनेंगे, मेरा भाषण करा दीजिए, हिन्दी विभाग में।’ लेखक के स्वाभिमान के विपरीत थी वह मुद्रा। ऊँची आवाज़ में मैंने उन्हें टोका- ‘‘पण्डितजी, हिन्दी विभाग के लिए यह गौरव की बात होगी कि आप वहाँ व्याख्यान दें। आपके प्रति यह विभागाध्यक्ष का अनुग्रह नहीं होगा।’’ प्रीत होकर उन्होंने कहा, ‘‘आप ही जैसे संस्कारी युवक पर समाज टिका हुआ है।’’ और चलते बने मगर उनकी बतकही ने मुझे भीतर से घायल कर दिया था। राह-घाट में कहीं दूर दिखाई पड़ते शान्तिप्रियजी तो बग़ल की राह पकड़कर उनकी संगति से बचने की कोशिश करने लगा था। एक दिन अस्सी चौमुनाही पर उन्होंने मुझे पकड़ लिया और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे-‘‘ द्विवेदीजी से बात कीजिए। छुट्टियाँ करीब हैं, फिर बात बिगड़ जाएगी ।’’
उनकी मुद्रा ने मेरे क्षोभ को फिर उत्तेजित किया। पर चुप लगा गया। अन्ततः उनकी साध हिन्दी विभागाध्यक्ष पं. हजारीप्रसाद द्विवेदी तक पहुँचाने की लाचारी थी। सुनते ही पण्डितजी ने अपनी सहज शैली में ज़ोर का ठहाका लगाया। फिर उनका आदेश था-‘‘डॉक्टर श्रीकृष्ण लालजी से बात करके समय तय कर लो और एक दिन शान्तिप्रियजी को विभाग में ले आओ।’’ लोलार्क कुण्ड से उन्हें हिन्दी विभाग में ले गया। छात्रों-अध्यापकों की संख्या बहुत कम थी। छात्राएँ और भी कम, नहीं के बराबर। कम उपस्थिति वक्ता को चिढ़ाने के लिए बहुत थी तथापि उन्होंने अपने ढंग से व्याख्यान दिया। पण्डित जी ने उनकी प्रशंसा में बहुत-कुछ-कहा, शिष्टाचारवश, अपने सहज कौशल के अनुरूप। पर द्विवेदी जी को बधिर माननेवाले पं. शान्तिप्रियजी ने पता नहीं कितना-कुछ सुना और उससे उनके मन का कितना समाधन हुआ। दो दिन बाद उनके गहरे असन्तोष का पता चला। मिलते ही कहने लगे-‘‘.....ने कक्षा से लड़कियों को अपने कूट कौशल से भगा दिया था। आप बहुत सीधे हैं। चालाकी समझ नहीं पाते। एक दूसरा कार्यक्रम कराइए, जिसमें छात्राएँ उपस्थित रहें। कार्यक्रम तय करके मुझे खबर दीजिए।’’
बड़ा संकट था, पण्डितजी के सामने फिर यह प्रसंग उठाना नहीं चाहिए था। शान्तिप्रियजी के हठ का क्या उपचार किया जाए ! पण्डित जी के व्यंजक ठहाका कई बार जटिल प्रसंग का समाधन कर देता था। उन्होंने सहज भाव से एक दिन पूछा, ‘‘कहो, पं. शान्तिप्रियजी का क्या हाल है ? अब तो तुष्ट हैं न ?’’ मेरा असमंजस टूट गया । मैंने उनकी शिकायत और आग्रह पण्डितजी के सामने जस-का-तस रख दिया। पण्डित जी ने बड़े ज़ोर का ठहाका लगाया !
काशी की प्रसिद्ध विद्या-विभूति पं. चन्द्रबली पाण्डेय यद्यपि विश्वविद्यालय सेवा से जुड़े थे, पर विश्वविद्यालय परिसर में ही अपने मित्र मौलवी महेश प्रसाद के साथ रहते थे। बाद में वे डॉ. ज्ञानवती त्रिवेदी के बँगले पर आ गये थे। पं. शान्तिप्रियजी और पं. चन्द्रबली पाण्डेय आजमगढ़ के विद्या-रत्न थे, और आजमगढ़ के राहुल सांकृत्यायन को अपने जनपत के पं. चन्द्रबली पाण्डेय, पं. लक्ष्मीनाराण मिश्र और पं. शान्तिप्रिय द्विवेदी की विद्या-साधना का सहज गर्व था। ‘अपनी जीवन-यात्रा में राहुलजी ने अपनी भावना प्रकट की है। हैदराबाद हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सन्दर्भ में, जिसके अध्यक्ष पं. चन्द्रबली पाण्डेय थे और सहित्य परिषद् के अध्यक्ष पं. लक्ष्मीनारायण मिश्र थे। मैंने शान्तिप्रियजी के प्रति राहुलजी की आत्मीयता देखी है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book