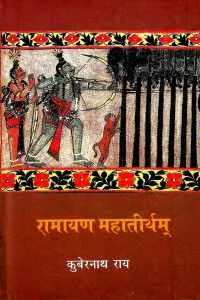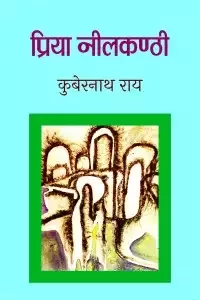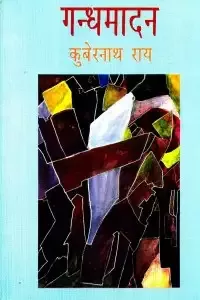|
लेख-निबंध >> रस आखेटक रस आखेटककुबेरनाथ राय
|
342 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है ललित निबन्ध...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
मनुष्य से ईश्वर तक सभी परस्पर आखेट-लीला में संलग्न है। यह आखेट लीला कभी
मधुर मोहक और कोमल दिखायी पड़ती है, तो कभी क्रूर प्राणघाती और आरण्यक !
किन्तु, अपने मूल-रूप में यह लीला एक द्वन्द्वातीत एवं निर्द्वन्द
प्रक्रिया है हमारे प्राण-स्तर और मन-स्तर निरन्तर व्यक्त होती हुई। यह
आखेट-लीला हमें विरोधी द्वन्द्वों के भ्रम देने लगती है, जब इसे हम अपने
अनुभव की सीमित क्षमता में परिमित करते हैं। किन्तु जब साहित्य एक समर्थ
माध्यम के रूप में हमारी अनुभूति को विस्तार देकर उस बिन्दु पर पहुँचा
देता है, जिस बिन्दु पर यह आखेट लीला अपने मूल रूप में है, तो हम पाते हैं
कि यह विशुद्ध ‘रस’ है-एक सहज निर्द्वन्द्व रसमयता।
‘रस-आखेटक’ के निबन्धकार ने रस की परिभाषा को एक नये आयाम में व्याख्यायित करने का प्रयत्न किया है। वह पाता है पुरानी पीढ़ी में सुन्दर के प्रति रोमाण्टिक मोह, तो नयी पीढ़ी में कदर्य और क्रुद्ध के प्रति रोमाण्टिक प्रतिबद्धता। इसलिए दोनों कूलों को अस्वीकार कर, इन निबन्धों में रस को मध्य-धार के बहते पानी का स्वस्थ और प्रसन्न-गम्भीर परिष्कार देने की चेष्टा की है सामर्थ्यवान प्रतिनिधि निबन्धकार कुबेरनाथ राय ने। रूप संरचना एवं प्रभावान्वित की दृष्टि से भी इन निबन्धों की संशिलष्ट निर्बन्धता अत्यत सघन रूप में सगुण और सटीक बन पड़ी है।
प्रस्तुत है ‘रस-आखेटक’ का यह नया संस्करण नये रूपाकार में।
‘रस-आखेटक’ के निबन्धकार ने रस की परिभाषा को एक नये आयाम में व्याख्यायित करने का प्रयत्न किया है। वह पाता है पुरानी पीढ़ी में सुन्दर के प्रति रोमाण्टिक मोह, तो नयी पीढ़ी में कदर्य और क्रुद्ध के प्रति रोमाण्टिक प्रतिबद्धता। इसलिए दोनों कूलों को अस्वीकार कर, इन निबन्धों में रस को मध्य-धार के बहते पानी का स्वस्थ और प्रसन्न-गम्भीर परिष्कार देने की चेष्टा की है सामर्थ्यवान प्रतिनिधि निबन्धकार कुबेरनाथ राय ने। रूप संरचना एवं प्रभावान्वित की दृष्टि से भी इन निबन्धों की संशिलष्ट निर्बन्धता अत्यत सघन रूप में सगुण और सटीक बन पड़ी है।
प्रस्तुत है ‘रस-आखेटक’ का यह नया संस्करण नये रूपाकार में।
भूमिका
रसोपनिषद्
अमृत का जन्म
अन्त में तय हुआ कि समुद्र मथकर अमृत निकाला जाए।
पहले तो वासुकि नाग अड़ गया कि वह अपनी देह की दुर्गति नहीं कराएगा। पर शिष्टमण्डल में जृम्भ और सुमाली जैसे क्रूर कर्मा दैत्य भी थे। अतः कुछ इनके डर से और कुछ इन्द्रियों के प्रभु इन्द्र के फुसलाने से अन्त में वह इच्छासर्प तैयार हो गया। सोचा कि चलो अमृत न सही अमृत का फेन चाटने का अवसर तो मिलेगा ही।
मेरु मन्दर की चापलूसी नहीं करनी पड़ी। साक्षात् स्थितप्रज्ञ कर्मयोगी की तरह गरिमावान् उस मेरु मन्दर को चापलूसी की क्या जरूरत ? वह प्रस्ताव करते ही राजी हो गया। पर उसने सवाल पेश किया ‘‘भाई तुम्हारे काम के लिए मैं इस पतित अपावन इच्छासर्प को अपनी देह में लपेटने के लिए तैयार हूँ। पर जैसे कर्मयोगी के लिए कोई स्थिर बिन्दु चाहिए वैसे ही मुझे भी कोई आधार चाहिए। तभी अमृत के लिए सागर मन्थन हो सकता है। मुझे आधार कौन देगा, इस वरुणालय के अतल गर्भ में ?’’
लोगों की नजरें मोटे-मोटे दैत्यों की ओर गयीं। पर शुक्राचार्य ने उपदेश दिया-‘‘यह काम इन लोगों के स्वभाव के विपरीत है। मन में आएगा तो उसी क्षण मन्दर-टन्दर फेंक-फाँक कर ये लोग अलग हो जाएँगे। इसके लिए कोई धीर आस्थावन् शान्त पुरुष चाहिए। हमारे यजमान लोग घर फूँक सकते हैं, लाठी चला सकते हैं। यह काम उनसे नहीं होगा।’’
अन्त में सबने मिलकर आस्थारूपिणी सरस्वती की प्रार्थना की। आकाश में नीलोपत्ल श्याम एक तेजस्वी कमठ पैदा हुआ। सारा आकाश तेज नीली रोशनी से ढँक गया। अन्त में तेज सिमटते-सिमटते एक तीक्ष्ण तीव्र प्रकाश का तीर बनकर समुद्र में प्रवेश कर गया। लहरें थम गयीं। आकाश से शब्द उत्पन्न हुए : ‘‘देवताओं और दानवों, स्वयं आस्थापुरुष ने कमठ बनकर अपनी बज्रोपम पीठ पर मन्दर ले लिया है। शाश्वत का रंग नीला होता है। तुम नील वर्ण शान्ताकारम् प्रभु का स्मरण करके मन्थन प्रारम्भ करो।’’
मेरु मन्दर ने अपने को धन्य माना ! इच्छा सर्प वासुकि खुद आकर उससे लिपट गया। इन्द्रादि देवतागण वासुकि के मुँह की ओर चले कि उसी समय सुमाली ने इन्द्र को ढकेल दिया और घुड़कते हुए कहा-‘दैत्य महाकुल कभी पूँछ पकड़ने वाला नहीं रहा है ? उधर तुम लोग जाओ !’’ इस प्रकार मन्थन का शुभारम्भ हुआ।
मन्थन करते-करते दोपहर हो चला। देव-मानव दोनों बदहवास हो चले। हवा थम गयी थी। सबका हाल बुरा था। मारे परिश्रम के एक-दूसरे से बोलने में भी कष्ट होता था। पर मन्थन रुका नहीं। चलता रहा। लगता था कि सारी सृष्टि हवा का बहना शब्दों की गति, फूल का खिलना पत्रों का बढ़ना सभी कुछ रुक गया है। शान्त मध्याह्न और परिपक्व वातावरण। लगता था कि किसी महान् क्षण का प्रसव होनेवाला है।
अचानक बड़े जोरों से फेन उठा। लगा कि कुछ समुद्र के भीतर से धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है। दोनों पक्षों ने रस्सी छोड़ दी। और अपनी आँखों को उसी दिशा में केन्द्रित कर लिया। वासुकि लपक-लपककर फेन चाट रहा था। शीतल झुरझुर बयार बहने लगी। वातावरण सुगन्ध से भर उठा। मस्तिष्क एक नशे, एक सम्मोहन में बंधकर लाचार हो गया मन्त्रविद्ध सर्प की तरह। कुछ क्षण बाद लहरों पर नृत्य करते हुए मयूर उठे। पुंज के पुंज कमल, अशोक, नवमल्लिका, नीलोत्पल और आम्रमंजरियाँ जलराशि पर तैरती बहती आने लगीं। वरुणालय का समस्त विस्तार फूलों से पट गया। वरुण स्रोतों पर तैरते फूलों के पुंज और नाचते मयूर। लगता था। कि समस्त सृष्टि एक अप्सरा है और गोपवेश विष्णु का रूप धारण करके दिशाओं के दस छिद्रों से काल की सम्मोहन वंशी बजा रही है।
बृहस्पति ने बताया-‘‘चन्द्रमा मनसो जातः। मन को मथने से चन्द्रमा पैदा होता है। यही रस और प्राण का सहचर है। इस समुद्र को मथने से आज हमें रसों में श्रेष्ठ श्रृंगार रस मिला है।’’
सबने अनुभव किया उनके मन में चन्द्रमा जैसे चेहरे देखे या अनदेखे डूब उतरा रहे हैं, वे लोग स्वप्नों के शिखर पर आरोहण कर रहे हैं, उन्हें नींद जैसी आ रही है।
धीरे-धीरे मोहिनी माया कटी। श्रृंगार रस अन्तर्धान हो गया। फिर मन्थन प्रारम्भ हुआ। इस बार वीर रस निकला। विशाल पर्वताकार तीन संयुक्त शिरों की त्रिमूर्ति धीरे-धीरे जल से ऊपर उठी और सामने स्थिर हो गयी। केवल शीर्ष भार ही शेष जलमग्न रहा। भयानक चेहरा वाला वाम शिर अघोर भैरव का था। दक्षिण शिर नील वर्ण रुद्र का था जिसके नयन-पल्लवों से क्रोध चू रहा था। मध्य शिर सौम्यशान्त गौरवर्ण दृढ़ होठ और निश्चय दीप्त भालवाले वीर रस के शिवमुख को देखकर सबने प्रमाण किया। धीरे-धीरे त्रिमूर्ति अन्तर्धान हो गयी। ‘भयानक और रौद्र’ के साथ ‘वीर’ का दर्शन करके इस नये रस-बोध से लोगों को लगा कि उनकी छाती और चौड़ी हो रही है, उनकी आत्मा विस्तार पा रही है, वे हिमालय पहाड़ का आलिंगन कर सकते हैं।
‘रस’ क्या था साक्षात् प्रतिज्ञा मूर्ति शिव ही थे। पर इसी रसावेश में कुछ के मन में हो रहा था कि यदि दुश्मन दिखाई पड़ जाय तो अभी गाली-गलोज शुरु कर दें। फिर हाथापाई।
फिर मन्थन। इस बार उदास कपोतवर्ण करुण रस का जन्म हुआ। वातावरण मेघाच्छन्न उदास हो गया। धूसरवर्णी अकेला कपोत, उसकी कोमल गरदन उसकी नरम पाँखें, उसके करुण दयनीय नेत्र आदि के दर्शन से घोर विषाद का अनुभव होता था। जन्म ही करुण है, प्रेम ही करुण है। विश्व का मूल ही करुण विषाद है ऐसे भावों से अचानक मन भर गया। भीतर कोई अनचीन्ही व्यथा मरोड़ने लगी। भीतर जो कुछ ठूँठ था, स्थाणु था या शिला की तरह अभिमानी था, विगलित होकर बहने लगा। सारा वन सूखे पत्तों से भर गया। वे पत्ते करुण रस से रो रहे थे। सबके मन में विषाद की वंशी बज उठी : ‘ओह धरती तूने जन्म क्यों दिया !’ ‘करुणानिधि जनार्दन, तुम कहाँ हो ?’ ‘हवाओं, तुम जाकर चकितनयना मृगशावक-सी मेरी वधू से कहना....’ ‘माँ, माँ तू हमें छोड़कर...’ विषाद् के स्वरों से सारी सृष्टि शोकमग्न हो गयी।
करुण रस की माया धीरे-धीरे कटी। अब दैत्यों को सब बेकार लग रहा था। दो-चार तो हटकर खड़े हो गये। ‘‘यार, सब बेकार हो ! दिन भर मथते रहे अमृत के नाम पर और ये सब फिजूल-फालतू चीजें निकल रही हैं।’’ ऐसी आवाजें उठने लगीं। पर दैत्यराज सुमाली ने सबको डाँटा-‘‘चलो, अपने काम पर ! अमृत इस बार आ रहा है। तीन उड़ान के बाद तीतर पकड़ाई देता है, ऐसा नियम है। यह गूढ़ रहस्य तुम लोग क्या जानोगे ? गुरु शुक्राचार्य की पाठशाला में मैंने ही तीन बार फेल होकर इस नियम के मुताबिक चौथी बार दर्जा चार पास किया था।’’
अपनी तर्कयुक्त युक्तिपूर्ण डाँट के जरिये उसने सबको ठेल-ठालकर मोड़ते पर खड़ा किया। फिर मन्थन शुरू हुआ। घनघोर मन्थन हुआ। साँझ हो आयी तो अद्भुत, हास और बीभत्स रस प्रकट हुए। बीभत्स के निकलते ही सबका जी मिचलाने लगा ! लगा कि पैरों के नीचे और चारों तरफ लिजलिजे दीन निरीह पर घृणित केंचुए रेंग रहे हैं। दुर्गन्ध और अरुचि से मन भर गया। उबकाई सी आने लगी। राजाधिराज अभिजात झाड़कर चल दिये। दैत्य पहले ही अलग हो चुके थे। इच्छा सर्प वासुकि भी अलग हो गया। ‘‘मैं ऐसे अमृत को पीकर अपने कलात्मक संस्कार नष्ट नहीं करूँगा। उफ् क्या दुर्गन्ध है।’’ कहकर चलता बना।
इधर दैत्यगण अपने बूढ़े पुरोहित शुक्राचार्य को बुरा-भला कह रहे थे।
‘‘छिः इसीलिए मेहनत करवाये। बूढ़े हो गये, अक्ल नहीं आयी !’’
‘‘हम सबको पशुओं की तरह नाधकर घोर परिश्रम करवाया और अपने किनारे बैठकर बृहस्पति के साथ सुरती खाते रहे।’’
‘‘पता चलता तब, जब दिन भर यह रस्सा खींचना पड़ता !’’
‘‘अरे ये पुरोहित हैं कि हम लोगों का सिर्फ अन्न खराब करने के लिए हैं।’’
बेचारे शुक्राचार्य अपने उद्दण्ड शिष्यों को अपनी सफाई देने का अवसर ही नहीं पा रहे थे।
इसी समय मेरु मन्दर ने गम्भीर स्वर में कहा-‘‘मैं जानता था अमृत नहीं मिलेगा। पर पहले कहता तो तुम कहते कि कतरा रहा हूँ !...देवताओं और दानवों, मन्थन कर्म है। कर्म से ‘रस’ मिलता है ‘अमृत’ नहीं। अमृत के पाने का माध्यम आशीर्वाद है, कर्म नहीं। अमृत नहीं मिला, न मिले। अमृत का सहोदर रस मिल गया। श्रृंगार, वीर, भयानक, रौद्र, करुण, अद्भुत, हास और बीभत्स। ‘रस’ अमृत का ही सहोदर है। अतः सन्तोष करो। कम नहीं मिला।’’
मेरु ने गुरु गम्भीर स्वर में फिर कहा-‘‘अमृत तो आशीर्वाद है। उसे अपने हृदय में पाओगे। यदि चाहो तो धीरे-धीरे उत्पल की तरह तुम्हारे अन्दर वह विकसित होगा। इसकी पवित्र गन्ध से तुम्हारा सम्पूर्ण जीवन भर जाएगा। यह तुम्हारे जन्म-जन्मान्तर के जहर को धीरे-धीरे खींचते हुए स्वतः श्याम वर्ण का हो जाएगा। तुम्हारे अन्दर तुम्हारे अनेक रिपु हैं। वे रिपु तुम्हारे क्रुद्ध मर्महीन कठोर अभिशप्त अनजिये व्यक्तित्व के ही चेहरे हैं। जिन्हें तुम गढ़ते हो और भूल जाते हो। पर वे रिपु बनकर तुम्हारे भीतर बैठे हैं, घात लगाये हैं। तुम उन रिपुओं को मार नहीं सकते, पर अमृत की गन्ध से उन्हें सुला सकते हो, उन्हें शिशुओं जैसा कोमल सुकुमार बना सकते हो।’’ कहकर मेरु मन्दर चुप हो गया।
सभी अपने-अपने घर चले गये। ...और इधर पाताललोक में-
दो सम्भ्रान्त सज्जन बात कर रहे थे। ‘‘अरे भाई शेष, कहाँ चले ? मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था।’’ अपनी वीणा पर हाथ फेरते एक ने दूसरे से कहा।
‘‘जा रहा हूँ जरा वासुकि के पास। अमृत मन्थन का क्या समाचार है जानने के लिए।
‘‘तो मुझी से सुन लो। अमृत नहीं मिला। सब बकवास था !’’ वीणाधारी ने कहा।
‘‘ऐसा ?’’
‘‘हाँ, पर एक बात सुनो कोई जाने न ! गुह्यातिगुह्यं इदम्। पिता ने देवलोक में सिर्फ मुझे ही बताया है। ...अमृत का जन्म हो रहा है, सगुण रूप में, भाव-बोध बनकर, द्वापर के अन्त में।’’ कहते समय वीणाधारी की आँखें बड़ी और बड़ी होती गयीं। ‘‘द्वापर के अन्त में ? कहाँ पर ?’’ शेषनाग ने चकित होकर पूछा।
‘‘वृन्दावन में...और आश्चर्य देवों नहीं मनुष्यों के माध्यम से यह व्यक्त होगा ?’’
पहले तो वासुकि नाग अड़ गया कि वह अपनी देह की दुर्गति नहीं कराएगा। पर शिष्टमण्डल में जृम्भ और सुमाली जैसे क्रूर कर्मा दैत्य भी थे। अतः कुछ इनके डर से और कुछ इन्द्रियों के प्रभु इन्द्र के फुसलाने से अन्त में वह इच्छासर्प तैयार हो गया। सोचा कि चलो अमृत न सही अमृत का फेन चाटने का अवसर तो मिलेगा ही।
मेरु मन्दर की चापलूसी नहीं करनी पड़ी। साक्षात् स्थितप्रज्ञ कर्मयोगी की तरह गरिमावान् उस मेरु मन्दर को चापलूसी की क्या जरूरत ? वह प्रस्ताव करते ही राजी हो गया। पर उसने सवाल पेश किया ‘‘भाई तुम्हारे काम के लिए मैं इस पतित अपावन इच्छासर्प को अपनी देह में लपेटने के लिए तैयार हूँ। पर जैसे कर्मयोगी के लिए कोई स्थिर बिन्दु चाहिए वैसे ही मुझे भी कोई आधार चाहिए। तभी अमृत के लिए सागर मन्थन हो सकता है। मुझे आधार कौन देगा, इस वरुणालय के अतल गर्भ में ?’’
लोगों की नजरें मोटे-मोटे दैत्यों की ओर गयीं। पर शुक्राचार्य ने उपदेश दिया-‘‘यह काम इन लोगों के स्वभाव के विपरीत है। मन में आएगा तो उसी क्षण मन्दर-टन्दर फेंक-फाँक कर ये लोग अलग हो जाएँगे। इसके लिए कोई धीर आस्थावन् शान्त पुरुष चाहिए। हमारे यजमान लोग घर फूँक सकते हैं, लाठी चला सकते हैं। यह काम उनसे नहीं होगा।’’
अन्त में सबने मिलकर आस्थारूपिणी सरस्वती की प्रार्थना की। आकाश में नीलोपत्ल श्याम एक तेजस्वी कमठ पैदा हुआ। सारा आकाश तेज नीली रोशनी से ढँक गया। अन्त में तेज सिमटते-सिमटते एक तीक्ष्ण तीव्र प्रकाश का तीर बनकर समुद्र में प्रवेश कर गया। लहरें थम गयीं। आकाश से शब्द उत्पन्न हुए : ‘‘देवताओं और दानवों, स्वयं आस्थापुरुष ने कमठ बनकर अपनी बज्रोपम पीठ पर मन्दर ले लिया है। शाश्वत का रंग नीला होता है। तुम नील वर्ण शान्ताकारम् प्रभु का स्मरण करके मन्थन प्रारम्भ करो।’’
मेरु मन्दर ने अपने को धन्य माना ! इच्छा सर्प वासुकि खुद आकर उससे लिपट गया। इन्द्रादि देवतागण वासुकि के मुँह की ओर चले कि उसी समय सुमाली ने इन्द्र को ढकेल दिया और घुड़कते हुए कहा-‘दैत्य महाकुल कभी पूँछ पकड़ने वाला नहीं रहा है ? उधर तुम लोग जाओ !’’ इस प्रकार मन्थन का शुभारम्भ हुआ।
मन्थन करते-करते दोपहर हो चला। देव-मानव दोनों बदहवास हो चले। हवा थम गयी थी। सबका हाल बुरा था। मारे परिश्रम के एक-दूसरे से बोलने में भी कष्ट होता था। पर मन्थन रुका नहीं। चलता रहा। लगता था कि सारी सृष्टि हवा का बहना शब्दों की गति, फूल का खिलना पत्रों का बढ़ना सभी कुछ रुक गया है। शान्त मध्याह्न और परिपक्व वातावरण। लगता था कि किसी महान् क्षण का प्रसव होनेवाला है।
अचानक बड़े जोरों से फेन उठा। लगा कि कुछ समुद्र के भीतर से धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है। दोनों पक्षों ने रस्सी छोड़ दी। और अपनी आँखों को उसी दिशा में केन्द्रित कर लिया। वासुकि लपक-लपककर फेन चाट रहा था। शीतल झुरझुर बयार बहने लगी। वातावरण सुगन्ध से भर उठा। मस्तिष्क एक नशे, एक सम्मोहन में बंधकर लाचार हो गया मन्त्रविद्ध सर्प की तरह। कुछ क्षण बाद लहरों पर नृत्य करते हुए मयूर उठे। पुंज के पुंज कमल, अशोक, नवमल्लिका, नीलोत्पल और आम्रमंजरियाँ जलराशि पर तैरती बहती आने लगीं। वरुणालय का समस्त विस्तार फूलों से पट गया। वरुण स्रोतों पर तैरते फूलों के पुंज और नाचते मयूर। लगता था। कि समस्त सृष्टि एक अप्सरा है और गोपवेश विष्णु का रूप धारण करके दिशाओं के दस छिद्रों से काल की सम्मोहन वंशी बजा रही है।
बृहस्पति ने बताया-‘‘चन्द्रमा मनसो जातः। मन को मथने से चन्द्रमा पैदा होता है। यही रस और प्राण का सहचर है। इस समुद्र को मथने से आज हमें रसों में श्रेष्ठ श्रृंगार रस मिला है।’’
सबने अनुभव किया उनके मन में चन्द्रमा जैसे चेहरे देखे या अनदेखे डूब उतरा रहे हैं, वे लोग स्वप्नों के शिखर पर आरोहण कर रहे हैं, उन्हें नींद जैसी आ रही है।
धीरे-धीरे मोहिनी माया कटी। श्रृंगार रस अन्तर्धान हो गया। फिर मन्थन प्रारम्भ हुआ। इस बार वीर रस निकला। विशाल पर्वताकार तीन संयुक्त शिरों की त्रिमूर्ति धीरे-धीरे जल से ऊपर उठी और सामने स्थिर हो गयी। केवल शीर्ष भार ही शेष जलमग्न रहा। भयानक चेहरा वाला वाम शिर अघोर भैरव का था। दक्षिण शिर नील वर्ण रुद्र का था जिसके नयन-पल्लवों से क्रोध चू रहा था। मध्य शिर सौम्यशान्त गौरवर्ण दृढ़ होठ और निश्चय दीप्त भालवाले वीर रस के शिवमुख को देखकर सबने प्रमाण किया। धीरे-धीरे त्रिमूर्ति अन्तर्धान हो गयी। ‘भयानक और रौद्र’ के साथ ‘वीर’ का दर्शन करके इस नये रस-बोध से लोगों को लगा कि उनकी छाती और चौड़ी हो रही है, उनकी आत्मा विस्तार पा रही है, वे हिमालय पहाड़ का आलिंगन कर सकते हैं।
‘रस’ क्या था साक्षात् प्रतिज्ञा मूर्ति शिव ही थे। पर इसी रसावेश में कुछ के मन में हो रहा था कि यदि दुश्मन दिखाई पड़ जाय तो अभी गाली-गलोज शुरु कर दें। फिर हाथापाई।
फिर मन्थन। इस बार उदास कपोतवर्ण करुण रस का जन्म हुआ। वातावरण मेघाच्छन्न उदास हो गया। धूसरवर्णी अकेला कपोत, उसकी कोमल गरदन उसकी नरम पाँखें, उसके करुण दयनीय नेत्र आदि के दर्शन से घोर विषाद का अनुभव होता था। जन्म ही करुण है, प्रेम ही करुण है। विश्व का मूल ही करुण विषाद है ऐसे भावों से अचानक मन भर गया। भीतर कोई अनचीन्ही व्यथा मरोड़ने लगी। भीतर जो कुछ ठूँठ था, स्थाणु था या शिला की तरह अभिमानी था, विगलित होकर बहने लगा। सारा वन सूखे पत्तों से भर गया। वे पत्ते करुण रस से रो रहे थे। सबके मन में विषाद की वंशी बज उठी : ‘ओह धरती तूने जन्म क्यों दिया !’ ‘करुणानिधि जनार्दन, तुम कहाँ हो ?’ ‘हवाओं, तुम जाकर चकितनयना मृगशावक-सी मेरी वधू से कहना....’ ‘माँ, माँ तू हमें छोड़कर...’ विषाद् के स्वरों से सारी सृष्टि शोकमग्न हो गयी।
करुण रस की माया धीरे-धीरे कटी। अब दैत्यों को सब बेकार लग रहा था। दो-चार तो हटकर खड़े हो गये। ‘‘यार, सब बेकार हो ! दिन भर मथते रहे अमृत के नाम पर और ये सब फिजूल-फालतू चीजें निकल रही हैं।’’ ऐसी आवाजें उठने लगीं। पर दैत्यराज सुमाली ने सबको डाँटा-‘‘चलो, अपने काम पर ! अमृत इस बार आ रहा है। तीन उड़ान के बाद तीतर पकड़ाई देता है, ऐसा नियम है। यह गूढ़ रहस्य तुम लोग क्या जानोगे ? गुरु शुक्राचार्य की पाठशाला में मैंने ही तीन बार फेल होकर इस नियम के मुताबिक चौथी बार दर्जा चार पास किया था।’’
अपनी तर्कयुक्त युक्तिपूर्ण डाँट के जरिये उसने सबको ठेल-ठालकर मोड़ते पर खड़ा किया। फिर मन्थन शुरू हुआ। घनघोर मन्थन हुआ। साँझ हो आयी तो अद्भुत, हास और बीभत्स रस प्रकट हुए। बीभत्स के निकलते ही सबका जी मिचलाने लगा ! लगा कि पैरों के नीचे और चारों तरफ लिजलिजे दीन निरीह पर घृणित केंचुए रेंग रहे हैं। दुर्गन्ध और अरुचि से मन भर गया। उबकाई सी आने लगी। राजाधिराज अभिजात झाड़कर चल दिये। दैत्य पहले ही अलग हो चुके थे। इच्छा सर्प वासुकि भी अलग हो गया। ‘‘मैं ऐसे अमृत को पीकर अपने कलात्मक संस्कार नष्ट नहीं करूँगा। उफ् क्या दुर्गन्ध है।’’ कहकर चलता बना।
इधर दैत्यगण अपने बूढ़े पुरोहित शुक्राचार्य को बुरा-भला कह रहे थे।
‘‘छिः इसीलिए मेहनत करवाये। बूढ़े हो गये, अक्ल नहीं आयी !’’
‘‘हम सबको पशुओं की तरह नाधकर घोर परिश्रम करवाया और अपने किनारे बैठकर बृहस्पति के साथ सुरती खाते रहे।’’
‘‘पता चलता तब, जब दिन भर यह रस्सा खींचना पड़ता !’’
‘‘अरे ये पुरोहित हैं कि हम लोगों का सिर्फ अन्न खराब करने के लिए हैं।’’
बेचारे शुक्राचार्य अपने उद्दण्ड शिष्यों को अपनी सफाई देने का अवसर ही नहीं पा रहे थे।
इसी समय मेरु मन्दर ने गम्भीर स्वर में कहा-‘‘मैं जानता था अमृत नहीं मिलेगा। पर पहले कहता तो तुम कहते कि कतरा रहा हूँ !...देवताओं और दानवों, मन्थन कर्म है। कर्म से ‘रस’ मिलता है ‘अमृत’ नहीं। अमृत के पाने का माध्यम आशीर्वाद है, कर्म नहीं। अमृत नहीं मिला, न मिले। अमृत का सहोदर रस मिल गया। श्रृंगार, वीर, भयानक, रौद्र, करुण, अद्भुत, हास और बीभत्स। ‘रस’ अमृत का ही सहोदर है। अतः सन्तोष करो। कम नहीं मिला।’’
मेरु ने गुरु गम्भीर स्वर में फिर कहा-‘‘अमृत तो आशीर्वाद है। उसे अपने हृदय में पाओगे। यदि चाहो तो धीरे-धीरे उत्पल की तरह तुम्हारे अन्दर वह विकसित होगा। इसकी पवित्र गन्ध से तुम्हारा सम्पूर्ण जीवन भर जाएगा। यह तुम्हारे जन्म-जन्मान्तर के जहर को धीरे-धीरे खींचते हुए स्वतः श्याम वर्ण का हो जाएगा। तुम्हारे अन्दर तुम्हारे अनेक रिपु हैं। वे रिपु तुम्हारे क्रुद्ध मर्महीन कठोर अभिशप्त अनजिये व्यक्तित्व के ही चेहरे हैं। जिन्हें तुम गढ़ते हो और भूल जाते हो। पर वे रिपु बनकर तुम्हारे भीतर बैठे हैं, घात लगाये हैं। तुम उन रिपुओं को मार नहीं सकते, पर अमृत की गन्ध से उन्हें सुला सकते हो, उन्हें शिशुओं जैसा कोमल सुकुमार बना सकते हो।’’ कहकर मेरु मन्दर चुप हो गया।
सभी अपने-अपने घर चले गये। ...और इधर पाताललोक में-
दो सम्भ्रान्त सज्जन बात कर रहे थे। ‘‘अरे भाई शेष, कहाँ चले ? मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था।’’ अपनी वीणा पर हाथ फेरते एक ने दूसरे से कहा।
‘‘जा रहा हूँ जरा वासुकि के पास। अमृत मन्थन का क्या समाचार है जानने के लिए।
‘‘तो मुझी से सुन लो। अमृत नहीं मिला। सब बकवास था !’’ वीणाधारी ने कहा।
‘‘ऐसा ?’’
‘‘हाँ, पर एक बात सुनो कोई जाने न ! गुह्यातिगुह्यं इदम्। पिता ने देवलोक में सिर्फ मुझे ही बताया है। ...अमृत का जन्म हो रहा है, सगुण रूप में, भाव-बोध बनकर, द्वापर के अन्त में।’’ कहते समय वीणाधारी की आँखें बड़ी और बड़ी होती गयीं। ‘‘द्वापर के अन्त में ? कहाँ पर ?’’ शेषनाग ने चकित होकर पूछा।
‘‘वृन्दावन में...और आश्चर्य देवों नहीं मनुष्यों के माध्यम से यह व्यक्त होगा ?’’
ईश्वर के बाग में
तब आदम ने मुझे बताया-
‘‘ईश्वर के बाग में, मैं और ईभा, हम दोनों टहला करते थे। चारों ओर रजतवर्णीं फाख्ताओं का मीठा शोर गूँजता रहता था। वातावरण पर हल्की नीली आभा छायी रहती थी। स्वर्ग में दिन, सप्ताह, अयन, संवत्सर, युग या मन्वन्तर नहीं होते। एकरस शान्त स्निग्ध प्रकाश की छाया में वह काल का सनातन रूप वर्तमान रहता है। तब हम दोनों बिलकुल निर्वसन रहा करते थे। मैं सोचता था यह ईभा भी अजीब जानवर है। सदैव मेरे साथ रहती है। परम पिता कहते थे कि यह पहले मेरे दिल में ही थी। बाद में बाहर आ गयी; और कल्पवृक्ष के नीचे मैंने इसे एक दिन पाया। मैंने एक खूबसूरत जानवर समझकर प्यार करना शुरू कर दिया। और जानवरों से इसकी शक्ल मुझसे मिलती भी थी। सिर्फ दो-तीन जगह फर्क था।
‘‘प्रभु पिता कहते थे : ‘यह मेरे दिल से ही निकली है।’ ठीक ही कहते होंगे पिता के दिल से भी बहुत-सी चीजें निकली हैं। सारे फूल, सारी ओषधियाँ, ओषधियों का राजा चन्द्रमा, सारी सृष्टि ही पहले पिता के दिल में थी, बाद में पिता के मन समुद्र से ये सब एक-एक कर के बाहर आयीं। परम पिता का दिल आरोग्य का, अमृत का, पवित्रता का अक्षय भण्डार है। जिसे वे अपने दिल में ले लेते हैं, यही कारण है कि उसकी आत्मा के घाव भर जाते हैं।’’
‘‘ईश्वर के बाग में, मैं और ईभा, हम दोनों टहला करते थे। चारों ओर रजतवर्णीं फाख्ताओं का मीठा शोर गूँजता रहता था। वातावरण पर हल्की नीली आभा छायी रहती थी। स्वर्ग में दिन, सप्ताह, अयन, संवत्सर, युग या मन्वन्तर नहीं होते। एकरस शान्त स्निग्ध प्रकाश की छाया में वह काल का सनातन रूप वर्तमान रहता है। तब हम दोनों बिलकुल निर्वसन रहा करते थे। मैं सोचता था यह ईभा भी अजीब जानवर है। सदैव मेरे साथ रहती है। परम पिता कहते थे कि यह पहले मेरे दिल में ही थी। बाद में बाहर आ गयी; और कल्पवृक्ष के नीचे मैंने इसे एक दिन पाया। मैंने एक खूबसूरत जानवर समझकर प्यार करना शुरू कर दिया। और जानवरों से इसकी शक्ल मुझसे मिलती भी थी। सिर्फ दो-तीन जगह फर्क था।
‘‘प्रभु पिता कहते थे : ‘यह मेरे दिल से ही निकली है।’ ठीक ही कहते होंगे पिता के दिल से भी बहुत-सी चीजें निकली हैं। सारे फूल, सारी ओषधियाँ, ओषधियों का राजा चन्द्रमा, सारी सृष्टि ही पहले पिता के दिल में थी, बाद में पिता के मन समुद्र से ये सब एक-एक कर के बाहर आयीं। परम पिता का दिल आरोग्य का, अमृत का, पवित्रता का अक्षय भण्डार है। जिसे वे अपने दिल में ले लेते हैं, यही कारण है कि उसकी आत्मा के घाव भर जाते हैं।’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book