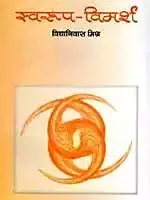|
लेख-निबंध >> स्वरूप-विमर्श स्वरूप-विमर्शविद्यानिवास मिश्र
|
124 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है सांस्कृतिक पर्यालोचन से सम्बद्ध निबन्धों का संकलन...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
कवि-नमन
नारायण पैदा होते रहे सदा नर में
कुछ महा-मानवों ने निश्चय
युग की पूजा स्वीकारी है
अपने चिन्तन से, कर्मों से, आचरणों से अवतारी बन, भवतारी बन, पैग़म्बर बन,
नर उन सबका आभारी है।
उन महर्षियों, युग-पुरुषों को
मेरे कवि के शत-शत प्रमाण!
कुछ महा-मानवों ने निश्चय
युग की पूजा स्वीकारी है
अपने चिन्तन से, कर्मों से, आचरणों से अवतारी बन, भवतारी बन, पैग़म्बर बन,
नर उन सबका आभारी है।
उन महर्षियों, युग-पुरुषों को
मेरे कवि के शत-शत प्रमाण!
मयूख’
प्राक्कथन
बांग्ला देश के मुक्ति-संघर्ष ने एक तथ्य बड़े ज़ोर से उजागर किया है कि
संस्कृ़ति कौम (राष्ट) की होती है, सम्प्रदाय की नहीं। मेरे विचार से
संस्कृति की जन्मपत्री में लिखा होना चाहिए कि एक भूखण्ड के निवासियों को
युग-पुरुष (समाज और राजनेता, सन्त साहित्यकार आदि) हज़ारों साल तक
प्रभावित करते हैं, तब कहीं जाकर इतिहास के गर्भ से उस कौंम की संस्कृति
का जन्म होता है।
हमारी भारतीय कौम की संस्कृति को जिन युग-पुरुषों क़ौम ने हजारों साल में ढाला हमारे पूर्वज हैं, हमारे साझे है। हमारे इतिहास-रथ की वल्गा कभी विश्वामित्र और अगस्त्य, युग-पुरुष राम और गीताकार कृष्ण ने थामी है तो कभी इस रथ पर आकार बैठ गये हैं राजपुरुष अशोक और अकबर। इस इतिहास-पथ पर खींच गये हैं सुनहरी लकीर कभी बुद्ध और महावीर नानक और कबीर, रसखान और जायसी, रहीम औऱ तुलसी, गालिब और रवीन्द्र, अरविन्द्र और विवेकानन्द दयान्नद, तुकाराम और चिश्ती एकनाथ और ज्ञानेश्वर और दक्षिण भारत के बहुत से सन्तों-साहित्यकारों सहित महामानव गाँधी।
इन सारे युग-पुरुषों का –सामाजिकों, राजनेताओं, सन्तों औऱ साहित्यकारों का-इतिहास हमारा इतिहास है। ये सब मिलकर हम यानी भारत राष्ट्र। और यहीं पर राष्ट्र और देश का अन्तर हो जाता है। हमारे भारत देश की भौगोलिक सीमा भले ही हिमालय से कन्याकुमारी तक रही हो, पर हमारे सांस्कृतिक राष्ट्र की सीमाएं और भी दूर-दूर तक फैली हुई है। (जिन्हें अन्ततोगत्वा मिलकतर महासंघ बनाना ही है)।
संस्कृति की परिवर्तनशीलता पर भौगोलिक दूरी टूटने का प्रभाव सतत पड़ता चला आ रहा है। इस प्रक्रिया का समापन निश्चय ही सारे विश्व को, इस पृथ्वी ग्रह के समस्त जन की, एक संस्कृति बनाने मानने में होगा1 जो आगे चलकर हजार-पाँच सौ सालों में अन्य ग्रहों पर उपस्थित संस्कृतियों से लेनदेन करेगी (इसकी
1. इसी स्थिति की कामना ऋग्वेद में है- समानी व आकूतिः-स्वर्णरेख, पृष्ठ 18
सम्भावना-घोषणा सैकड़ों प्रकाशवर्त दूरस्थ लोकों को टटोलने वाले विज्ञान ने कर दी है। संस्कृति को सम्प्रदाए के नाम पर छोटे-छोटे घेरों में घेरने की काल-विरोधी कोशिश गलत है। नकली घेरों को आज बांग्ला देश तोड़ रहा है। कल विश्व के अन्य देश तोडे़गे। अन्य में यह धारित्री या तो ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ बनेगी, अथवा नष्ट हो जाएगी। हजारों साल के गुजरे अतीत से जनमें हम हज़ारों साल आगे के भविष्य में क्यों झोंकें !
इनसान ने सपने देखना शुरू किया, हज़ारों साल पहले के अजीब सपने, हवा में उड़ने का सपना, मौत से ल़ड़ने का सपना, अन्तर्नक्षत्रीय यात्राओं का सपना, और भी अनेक अद्भुद सपने। मनुष्य जाति के हजारों साल के अन्तराल में ऐसे सपने बराबर देखे जाते चले आ रहे हैं। अश्विनीकुमारों के लौह-पग रोपण, मस्तक प्रतिरोपण से लेकर आधुनिक हृदय प्रतिरोपण तक मौत से लड़ने के सपने और प्रयास चले हैं-इसकी कथा हमारे पास है।
वैज्ञानिक सपनों की सम्भावनाओं एवं आध्यात्मिक दर्शनों से अलग हटकर भी यदि ऋग्वेद पर दृष्टि डाली जाए, तो भी इस पर मुग्ध हुए बिना नहीं रहा जा सकता चाहे इसे तत्कालीन समाज का इतिहास माना जाए अथवा काव्य-ग्रन्थ। सच तो यह है कि काव्य-साहित्य, इतिहास, भूगोग, विज्ञान, दर्शन अध्यात्म एवं भौतिकता का किसी एक ग्रन्थ में अवलोकन करना तो वह है ऋग्वेद।
ऋग्वेद से सम्बन्धित जो कुछ भी छिपपुट पढ़ता रहा उसमें मुझे अत्यन्त आकर्षण दिखा और उसने मेरी तृषा को बढ़ाया। तृषा की तृप्ति में तो मेरी आर्थिक अक्षमता ने रोड़े क्या चट्टानें अटकायीं किन्तु आकर्षण आख़िर जीत गया। मैंने पुस्तकों को टटोला, विद्वानों से विचार-विमर्श किये, फलस्वरूप प्रस्तुत कृति अस्तित्व में आयी। इसी उपक्रम में डॉ. रघुनाथ सिंह जी की कथा-पुस्तक ‘ऋग्वेद कथा’ देखने को मिली। ऋग्वेद की ऋचाओं के काव्य-लालित्य, कल्पना- प्रणवता और उपमा-सौन्दर्य पर तो मैं मुग्ध था ही, आदरणीय डॉ. साहब की काव्यमय शब्द-शैली मुझे और विभोर कर गयी। उनकी तीन कथाओं को काव्यरूप देने का मैं लोभ संवरण न कर पाया। उन्होंने इन कथाओं को इस रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति देने का मुझ पर अनुग्रह किया, एतदर्थ मैं उनका आभारी हूँ।
ऋग्वेद देखने पर कुछ बढ़िया बातों पर नज़र जाती है। आर्य-अनार्य (सुर-असुर) समाज का एक-दूसरे से बिलकुल विपरीत जीवन-दर्शन। इस भिन्नताओं की टकराहट जहाँ देवासुर-संग्रामों ‘दाशराज्ञ’ युद्धों में प्रकट हुई, वहाँ सांस्कृतिक समन्वयन के प्रयास भी इस सीमा तक चले कि दोनों समाज के विद्वान एक-दूसरे के पुरोहित तक बन गये। ऐसा लगता है कि शम्बर के पतन के पश्चात् विश्वामित्र इस समन्वयन के मुख्य उद्घोषक रहे।1 आर्य-अनार्य समाज में न केवल रोटी-व्यवहार बल्कि बेटी-व्यवहार तक चला। साथ ही तत्कालीन आर्य-अनार्य समाज ने एक-दूसरे के देवताओं (युग-पुरुषों) तक को मान्यता देकर स्वीकारा। तब से आज तक कितने ही ‘शंकर’ ज़हर पी गये, कितने ही चर्वाकों ने बग़ावत की हद तक समन्वय-स्वर मुखर किये-मनु की कट्टरता से पाराशर की उदारता तक का इतिहास इसका साक्षी है। आगे चलकर यह इतिहास कभी गांधी के सीने पर लिखी गया तो कभी बंगदेश के मस्तक पर।
दूसरी बात यह द्रष्टव्य है कि युद्धरत रहते हुए भी ऋग्वैदिक समाज का युद्ध-वर्जना का एक चिन्तन-दर्शन रहा2 पर युद्ध नहीं रुके, तब से आज तक नहीं रुके। ऋग्वेद के ऋचाकार से लेकर आइन्सटीन और गाँधी तक-सभी युद्ध को ग़लत बताते रहे, पर मनुष्य जाति के हज़ारों साल के ज्ञात इतिहास में आज तक एक हज़ार दिन भी ऐसे नहीं गिनाये जा सकते जब धरती पर युद्ध न हों। शम्बर दिवोदास के ‘दशायज्ञ’ युद्धों से लेकर क्रूसेड और जिहाद के मैदानों तक, हिटलर के अभियानों से लेकर बन्दूक़ की नली से सत्ता प्रकट करने के माओ के नारों, बांग्ला देश और वियतनाम के बलिदानों तक युद्ध का दर्शन ज़िन्दा रहा है।
अकसर ही ये युद्ध सम्प्रदाय और संस्कृति के झूठे नाम पर लड़े गये, यद्यपि सम्प्रदाय का संस्कृति से सीधा सम्बन्ध नहीं—जैसा कि मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया है संस्कृति राष्ट्र यानी क़ौम की होती है (अरब और भारत की संस्कृति में सम्प्रदाय के नाम पर समानता नहीं ढूँढ़ी जा सकती), फिर भी हुआ यह है कि सम्प्रदाय और संस्कृति के दो घोड़ों के रथ पर सवार होकर राजनीति ने इनसान के रक्त से धरती सींचकर युद्ध के दर्शन को ज़िन्दा रखा है। सांस्कृतिक क्रान्ति के नाम पर आज भी तिब्बत और चीन में जितना खून बहा उससे माओ की लाल किताब लाल है। भारत के ‘नक़ली’ बँटवारे के दौरान राजनीति ने इन्हीं झूठे नारे के नाम पर इनसानियत को कफ़न बाँटे थे। आज भी साम्प्रदायिक उन्माद में यही होता है।
युद्ध के इस दर्शन को कैसे झुठलाया जाए ? विश्व की इन संस्कृतियों का क्या हो—भारतीयकरण, रूसीकरण अथवा चीन-अमरीकीकरण ? चलने दी जाए देवासुर संग्रामों की सनातन असफल परम्परा ? या फिर इसके लिए सुदूर वैदिक काल में ही प्रारम्भ किये गये समन्वय प्रयासों से दिशा-दृष्टि से ? सांस्कृतिक भिन्नताओं के बावजूद एक-दूसरे के पुरोहित बनें, युग-पुरुषों को स्वीकारें, सामाजिक साम्य स्थापित करें ?
———————————
1.अदेदिष्ट वृत्तहा-विश्वा-अवृणोदय स्वाः—स्वर्णरेख, पृष्ठ 82
2. यात्रा नरः समयन्ते—स्वर्णरेख, पृष्ठ 84
जवाब ढूँढ़ना है रक्त-स्नात बूढ़े पृथ्वी ग्रह पर बसने वाले आज के विज्ञान-वेत्ता इनसान को—अहं ब्रह्मास्मि’ के उद्घोषक उस मनुष्य को कुरान की भाषा में ‘अशरफ़ुल-मख़लूकात’ (सृष्टि में सर्वेश्रेष्ठ) कहा गया है, उस इन्सान को जिसे आने वाले हज़ार-पाँच सौ सालों में अन्य ग्रहों पर उपस्थित संस्कृतियों से लेनदेन करना है।
मेरे वक्तव्य का प्रस्तुत काव्य से यद्यपि सम्बन्ध नहीं जुड़ता, फिर भी ऋग्वेद को जिस दृष्टि से मैंने देखा उसे आपके सामने रखना ज़रूरी समझा। ऋचाओं के आध्यात्मिक एवं दर्शन-पक्ष में भी अधिक न जाकर भौतिक अर्थ लेकर ही लिखी है। अथाह सागर से एक बूँद ही ले पाया हूँ। लेखन के दौरान प्रस्तुत विषय में अपने अज्ञान अल्पज्ञता की तीव्र अनुभूति से ग्रस्त रहा हूँ, अतः त्रुटिया के लिए क्षमा का अधिकारी भी। मन्त्रों के भाव को अपनी बुद्धिनुसार आत्मसात् करने के पश्चात् अपने शब्दों में काव्यरूप दिया है। अतः शब्दानुवाद नहीं है। इसकी एक विशेषता ने मेरा ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया है कि यह संसार के इस प्रकार के अन्य ग्रन्थों की भाँति एकमुखी न होकर अनेक मन्त्रद्रष्टा ऋषियों के मुख से उद्भूत हुआ है, अतः अपौरुषेय होकर भी अपने आप में जन-मुखी बन गया है। मैंने इस अलौकिक ग्रन्थ को लोक और समाज से सम्बन्द्ध करने की चेष्टा की है। विद्वान् समालोचकों को यदि इस दृष्टि से पीड़ा पहुँचे तो वे कृपया क्षमा करें।
अन्त में एक विनम्र निवेदन यह है कि मेरे परिवार की भाषा हिन्दी नहीं रही। भाई एवं पिता उर्दू-फ़ारसी में लिखते रहे। मैं हिंदी के माध्यम से आपके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। प्रस्तुत कृति में हो सकता है कि, भाषा का यह पारिवारिक परिवेश, जिसमें बचपन से पलता रहा, कहीं बोल उठा हो।
लेखन के दौरान दिशा-बोध देने से लेकर प्रस्तुत कृति आपके समक्ष पहुँचाने तक जिन विद्वानों का अजस्र आशीर्वाद मुझे मिलता रहा, उन्हें इस सन्दर्भ में कैसे विस्मृत करूँ। अतः आभारी हूँ राजस्थान के महाधिवक्ता डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघली एवं मेरी ही छात्रावस्था से मुझ पर अग्रज-सम स्नेह रखने वाले राजभाषा विधायी आयोग के सदस्य श्री नाथूलाल जैन का। मेरे कविमित्र भाई रामसिख मनहर एवं बालकवि प्रकाशवीर शास्त्री, गोपालप्रसाद व्यास, फतहचन्द आराधक, नरेन्द्र विद्यावाचस्पति, दिल्ली के महापौर माननीय केदारनाथ साहनी, राज्य कृषिमन्त्री माननीय प्रोफ़ेसर शेरसिंह जी, योग साधना आश्रम (जयपुर) के संचालक स्वामी आनन्दानन्द जी, राजस्थान मंच (दिल्ली) के श्री ए. भीष्मपाल एवं अनजान ने जो स्नेहाशीर्वाद दिये, उससे इस दिशा में और अधिक लिखने का आत्मविश्वास जागा है। एतदर्थ इन सब के प्रति हृदय के गहन तल से आन्तरिक कृतज्ञता अर्पित करता हूँ।
भारतीय ज्ञानपीठ ने इस कृति के प्रकाशन का दायित्व ग्रहण कर अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक चेतना और जागरुकता का परिचय दिया है, उसे नमन।
विज्ञजनों एवं हिन्दीभाषी समाज से समुचित दिशाबोध और स्नेहाशीर्वाद मिलने की कामना के साथ, अपने पुरखों की बात—स्वर्णरेख’ सविनय प्रस्तुत कर रहा हूँ।
हमारी भारतीय कौम की संस्कृति को जिन युग-पुरुषों क़ौम ने हजारों साल में ढाला हमारे पूर्वज हैं, हमारे साझे है। हमारे इतिहास-रथ की वल्गा कभी विश्वामित्र और अगस्त्य, युग-पुरुष राम और गीताकार कृष्ण ने थामी है तो कभी इस रथ पर आकार बैठ गये हैं राजपुरुष अशोक और अकबर। इस इतिहास-पथ पर खींच गये हैं सुनहरी लकीर कभी बुद्ध और महावीर नानक और कबीर, रसखान और जायसी, रहीम औऱ तुलसी, गालिब और रवीन्द्र, अरविन्द्र और विवेकानन्द दयान्नद, तुकाराम और चिश्ती एकनाथ और ज्ञानेश्वर और दक्षिण भारत के बहुत से सन्तों-साहित्यकारों सहित महामानव गाँधी।
इन सारे युग-पुरुषों का –सामाजिकों, राजनेताओं, सन्तों औऱ साहित्यकारों का-इतिहास हमारा इतिहास है। ये सब मिलकर हम यानी भारत राष्ट्र। और यहीं पर राष्ट्र और देश का अन्तर हो जाता है। हमारे भारत देश की भौगोलिक सीमा भले ही हिमालय से कन्याकुमारी तक रही हो, पर हमारे सांस्कृतिक राष्ट्र की सीमाएं और भी दूर-दूर तक फैली हुई है। (जिन्हें अन्ततोगत्वा मिलकतर महासंघ बनाना ही है)।
संस्कृति की परिवर्तनशीलता पर भौगोलिक दूरी टूटने का प्रभाव सतत पड़ता चला आ रहा है। इस प्रक्रिया का समापन निश्चय ही सारे विश्व को, इस पृथ्वी ग्रह के समस्त जन की, एक संस्कृति बनाने मानने में होगा1 जो आगे चलकर हजार-पाँच सौ सालों में अन्य ग्रहों पर उपस्थित संस्कृतियों से लेनदेन करेगी (इसकी
1. इसी स्थिति की कामना ऋग्वेद में है- समानी व आकूतिः-स्वर्णरेख, पृष्ठ 18
सम्भावना-घोषणा सैकड़ों प्रकाशवर्त दूरस्थ लोकों को टटोलने वाले विज्ञान ने कर दी है। संस्कृति को सम्प्रदाए के नाम पर छोटे-छोटे घेरों में घेरने की काल-विरोधी कोशिश गलत है। नकली घेरों को आज बांग्ला देश तोड़ रहा है। कल विश्व के अन्य देश तोडे़गे। अन्य में यह धारित्री या तो ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ बनेगी, अथवा नष्ट हो जाएगी। हजारों साल के गुजरे अतीत से जनमें हम हज़ारों साल आगे के भविष्य में क्यों झोंकें !
इनसान ने सपने देखना शुरू किया, हज़ारों साल पहले के अजीब सपने, हवा में उड़ने का सपना, मौत से ल़ड़ने का सपना, अन्तर्नक्षत्रीय यात्राओं का सपना, और भी अनेक अद्भुद सपने। मनुष्य जाति के हजारों साल के अन्तराल में ऐसे सपने बराबर देखे जाते चले आ रहे हैं। अश्विनीकुमारों के लौह-पग रोपण, मस्तक प्रतिरोपण से लेकर आधुनिक हृदय प्रतिरोपण तक मौत से लड़ने के सपने और प्रयास चले हैं-इसकी कथा हमारे पास है।
वैज्ञानिक सपनों की सम्भावनाओं एवं आध्यात्मिक दर्शनों से अलग हटकर भी यदि ऋग्वेद पर दृष्टि डाली जाए, तो भी इस पर मुग्ध हुए बिना नहीं रहा जा सकता चाहे इसे तत्कालीन समाज का इतिहास माना जाए अथवा काव्य-ग्रन्थ। सच तो यह है कि काव्य-साहित्य, इतिहास, भूगोग, विज्ञान, दर्शन अध्यात्म एवं भौतिकता का किसी एक ग्रन्थ में अवलोकन करना तो वह है ऋग्वेद।
ऋग्वेद से सम्बन्धित जो कुछ भी छिपपुट पढ़ता रहा उसमें मुझे अत्यन्त आकर्षण दिखा और उसने मेरी तृषा को बढ़ाया। तृषा की तृप्ति में तो मेरी आर्थिक अक्षमता ने रोड़े क्या चट्टानें अटकायीं किन्तु आकर्षण आख़िर जीत गया। मैंने पुस्तकों को टटोला, विद्वानों से विचार-विमर्श किये, फलस्वरूप प्रस्तुत कृति अस्तित्व में आयी। इसी उपक्रम में डॉ. रघुनाथ सिंह जी की कथा-पुस्तक ‘ऋग्वेद कथा’ देखने को मिली। ऋग्वेद की ऋचाओं के काव्य-लालित्य, कल्पना- प्रणवता और उपमा-सौन्दर्य पर तो मैं मुग्ध था ही, आदरणीय डॉ. साहब की काव्यमय शब्द-शैली मुझे और विभोर कर गयी। उनकी तीन कथाओं को काव्यरूप देने का मैं लोभ संवरण न कर पाया। उन्होंने इन कथाओं को इस रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति देने का मुझ पर अनुग्रह किया, एतदर्थ मैं उनका आभारी हूँ।
ऋग्वेद देखने पर कुछ बढ़िया बातों पर नज़र जाती है। आर्य-अनार्य (सुर-असुर) समाज का एक-दूसरे से बिलकुल विपरीत जीवन-दर्शन। इस भिन्नताओं की टकराहट जहाँ देवासुर-संग्रामों ‘दाशराज्ञ’ युद्धों में प्रकट हुई, वहाँ सांस्कृतिक समन्वयन के प्रयास भी इस सीमा तक चले कि दोनों समाज के विद्वान एक-दूसरे के पुरोहित तक बन गये। ऐसा लगता है कि शम्बर के पतन के पश्चात् विश्वामित्र इस समन्वयन के मुख्य उद्घोषक रहे।1 आर्य-अनार्य समाज में न केवल रोटी-व्यवहार बल्कि बेटी-व्यवहार तक चला। साथ ही तत्कालीन आर्य-अनार्य समाज ने एक-दूसरे के देवताओं (युग-पुरुषों) तक को मान्यता देकर स्वीकारा। तब से आज तक कितने ही ‘शंकर’ ज़हर पी गये, कितने ही चर्वाकों ने बग़ावत की हद तक समन्वय-स्वर मुखर किये-मनु की कट्टरता से पाराशर की उदारता तक का इतिहास इसका साक्षी है। आगे चलकर यह इतिहास कभी गांधी के सीने पर लिखी गया तो कभी बंगदेश के मस्तक पर।
दूसरी बात यह द्रष्टव्य है कि युद्धरत रहते हुए भी ऋग्वैदिक समाज का युद्ध-वर्जना का एक चिन्तन-दर्शन रहा2 पर युद्ध नहीं रुके, तब से आज तक नहीं रुके। ऋग्वेद के ऋचाकार से लेकर आइन्सटीन और गाँधी तक-सभी युद्ध को ग़लत बताते रहे, पर मनुष्य जाति के हज़ारों साल के ज्ञात इतिहास में आज तक एक हज़ार दिन भी ऐसे नहीं गिनाये जा सकते जब धरती पर युद्ध न हों। शम्बर दिवोदास के ‘दशायज्ञ’ युद्धों से लेकर क्रूसेड और जिहाद के मैदानों तक, हिटलर के अभियानों से लेकर बन्दूक़ की नली से सत्ता प्रकट करने के माओ के नारों, बांग्ला देश और वियतनाम के बलिदानों तक युद्ध का दर्शन ज़िन्दा रहा है।
अकसर ही ये युद्ध सम्प्रदाय और संस्कृति के झूठे नाम पर लड़े गये, यद्यपि सम्प्रदाय का संस्कृति से सीधा सम्बन्ध नहीं—जैसा कि मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया है संस्कृति राष्ट्र यानी क़ौम की होती है (अरब और भारत की संस्कृति में सम्प्रदाय के नाम पर समानता नहीं ढूँढ़ी जा सकती), फिर भी हुआ यह है कि सम्प्रदाय और संस्कृति के दो घोड़ों के रथ पर सवार होकर राजनीति ने इनसान के रक्त से धरती सींचकर युद्ध के दर्शन को ज़िन्दा रखा है। सांस्कृतिक क्रान्ति के नाम पर आज भी तिब्बत और चीन में जितना खून बहा उससे माओ की लाल किताब लाल है। भारत के ‘नक़ली’ बँटवारे के दौरान राजनीति ने इन्हीं झूठे नारे के नाम पर इनसानियत को कफ़न बाँटे थे। आज भी साम्प्रदायिक उन्माद में यही होता है।
युद्ध के इस दर्शन को कैसे झुठलाया जाए ? विश्व की इन संस्कृतियों का क्या हो—भारतीयकरण, रूसीकरण अथवा चीन-अमरीकीकरण ? चलने दी जाए देवासुर संग्रामों की सनातन असफल परम्परा ? या फिर इसके लिए सुदूर वैदिक काल में ही प्रारम्भ किये गये समन्वय प्रयासों से दिशा-दृष्टि से ? सांस्कृतिक भिन्नताओं के बावजूद एक-दूसरे के पुरोहित बनें, युग-पुरुषों को स्वीकारें, सामाजिक साम्य स्थापित करें ?
———————————
1.अदेदिष्ट वृत्तहा-विश्वा-अवृणोदय स्वाः—स्वर्णरेख, पृष्ठ 82
2. यात्रा नरः समयन्ते—स्वर्णरेख, पृष्ठ 84
जवाब ढूँढ़ना है रक्त-स्नात बूढ़े पृथ्वी ग्रह पर बसने वाले आज के विज्ञान-वेत्ता इनसान को—अहं ब्रह्मास्मि’ के उद्घोषक उस मनुष्य को कुरान की भाषा में ‘अशरफ़ुल-मख़लूकात’ (सृष्टि में सर्वेश्रेष्ठ) कहा गया है, उस इन्सान को जिसे आने वाले हज़ार-पाँच सौ सालों में अन्य ग्रहों पर उपस्थित संस्कृतियों से लेनदेन करना है।
मेरे वक्तव्य का प्रस्तुत काव्य से यद्यपि सम्बन्ध नहीं जुड़ता, फिर भी ऋग्वेद को जिस दृष्टि से मैंने देखा उसे आपके सामने रखना ज़रूरी समझा। ऋचाओं के आध्यात्मिक एवं दर्शन-पक्ष में भी अधिक न जाकर भौतिक अर्थ लेकर ही लिखी है। अथाह सागर से एक बूँद ही ले पाया हूँ। लेखन के दौरान प्रस्तुत विषय में अपने अज्ञान अल्पज्ञता की तीव्र अनुभूति से ग्रस्त रहा हूँ, अतः त्रुटिया के लिए क्षमा का अधिकारी भी। मन्त्रों के भाव को अपनी बुद्धिनुसार आत्मसात् करने के पश्चात् अपने शब्दों में काव्यरूप दिया है। अतः शब्दानुवाद नहीं है। इसकी एक विशेषता ने मेरा ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया है कि यह संसार के इस प्रकार के अन्य ग्रन्थों की भाँति एकमुखी न होकर अनेक मन्त्रद्रष्टा ऋषियों के मुख से उद्भूत हुआ है, अतः अपौरुषेय होकर भी अपने आप में जन-मुखी बन गया है। मैंने इस अलौकिक ग्रन्थ को लोक और समाज से सम्बन्द्ध करने की चेष्टा की है। विद्वान् समालोचकों को यदि इस दृष्टि से पीड़ा पहुँचे तो वे कृपया क्षमा करें।
अन्त में एक विनम्र निवेदन यह है कि मेरे परिवार की भाषा हिन्दी नहीं रही। भाई एवं पिता उर्दू-फ़ारसी में लिखते रहे। मैं हिंदी के माध्यम से आपके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। प्रस्तुत कृति में हो सकता है कि, भाषा का यह पारिवारिक परिवेश, जिसमें बचपन से पलता रहा, कहीं बोल उठा हो।
लेखन के दौरान दिशा-बोध देने से लेकर प्रस्तुत कृति आपके समक्ष पहुँचाने तक जिन विद्वानों का अजस्र आशीर्वाद मुझे मिलता रहा, उन्हें इस सन्दर्भ में कैसे विस्मृत करूँ। अतः आभारी हूँ राजस्थान के महाधिवक्ता डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघली एवं मेरी ही छात्रावस्था से मुझ पर अग्रज-सम स्नेह रखने वाले राजभाषा विधायी आयोग के सदस्य श्री नाथूलाल जैन का। मेरे कविमित्र भाई रामसिख मनहर एवं बालकवि प्रकाशवीर शास्त्री, गोपालप्रसाद व्यास, फतहचन्द आराधक, नरेन्द्र विद्यावाचस्पति, दिल्ली के महापौर माननीय केदारनाथ साहनी, राज्य कृषिमन्त्री माननीय प्रोफ़ेसर शेरसिंह जी, योग साधना आश्रम (जयपुर) के संचालक स्वामी आनन्दानन्द जी, राजस्थान मंच (दिल्ली) के श्री ए. भीष्मपाल एवं अनजान ने जो स्नेहाशीर्वाद दिये, उससे इस दिशा में और अधिक लिखने का आत्मविश्वास जागा है। एतदर्थ इन सब के प्रति हृदय के गहन तल से आन्तरिक कृतज्ञता अर्पित करता हूँ।
भारतीय ज्ञानपीठ ने इस कृति के प्रकाशन का दायित्व ग्रहण कर अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक चेतना और जागरुकता का परिचय दिया है, उसे नमन।
विज्ञजनों एवं हिन्दीभाषी समाज से समुचित दिशाबोध और स्नेहाशीर्वाद मिलने की कामना के साथ, अपने पुरखों की बात—स्वर्णरेख’ सविनय प्रस्तुत कर रहा हूँ।
-बशीर अहमद ‘मयूख’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book