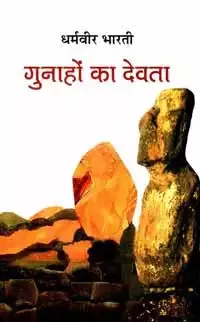|
आलोचना >> मानव मूल्य और साहित्य मानव मूल्य और साहित्यधर्मवीर भारती
|
369 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत है मानव मूल्य और साहित्य...
Manav mulya aur sahitya
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘‘सांस्कृतिक संकट या मानवीय तत्त्व के विघटन की जो बात बहुधा उठायी जाती रही है उसका तात्पर्य यही रहा है कि वर्तमान युग में ऐसी परिस्थियाँ उत्पन्न हो चुकी है जिनमें अपनी नियति के इतिहास निर्माण के सूत्र मनुष्य के हाथों से छूटे हुए लगते हैं। मनुष्य दिनों-दिन निरर्थकता की ओर अग्रसर होता प्रतीत होता है। यह संकट केवल आर्थिक और राजनीतिक संकट नहीं है वरन् जीवन के सभी पक्षों में समान रूप से प्रतिफलित हो रहा है। यह संकट केवल पश्चिम या पूर्व का नहीं है वरन् समस्त संसार में विभिन्न धरातलों पर विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है।’’
भूमिका
(प्रथम संस्करण से)
जब हम मानव मूल्य की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य क्या है, यह समझ लेना आवश्यक है। अपनी परिस्थितियाँ, इतिहास-क्रम और काल-प्रवाह के सन्दर्भ में मनुष्य की स्थिति क्या है और महत्त्व क्या है-वास्तविक समस्या इस बिन्दु से उठती है। समस्त मध्यकाल में इस निखिल सृष्टि और इतिहास-क्रम का नियन्ता किसी मानवोपरि अलौकिक सत्ता को माना जाता था। समस्त मूल्यों का स्रोत्र वही था और मनुष्य की एक मात्र सार्थकता यही थी कि वह अधिक से अधिक उस सत्ता से तादात्म्य स्थापित करने की चेष्टा करे। इतिहास या काल-प्रवाह उसी मानवोपरि सत्ता की सृष्टि था-माया रूप में या लीला रूप में।
ज्यों-ज्यों हम आधुनिक युग में प्रवेश करते गये त्यों-त्यों इस मानवोपरि सत्ता का अवमूल्यन होता गया। मनुष्य की गरिमा का नये स्तर पर उदय हुआ और माना जाने लगा कि मनुष्य अपने में स्वत: सार्थक और मूल्यवान् है-वह आन्तरिक शक्तियों से संपन्न, चेतन-स्तर पर अपनी नियति के निर्माण के लिए स्वत: निर्णय लेने वाला प्राणी है। सृष्टि के केन्द्र में मनुष्य है। यह भावना बीच-बीच में मध्यकाल के साधकों या सन्तों में भी कभी-कभी उदित हुई थी, किन्तु आधुनिक युग के पहले यह कभी सर्वमान्य नहीं हो पायी थी।
लेकिन जहाँ तक एक ओर सिद्धांतों के स्तर पर मनुष्य की सार्वभौमिक सर्वोपरि सत्ता स्थापित हुई, वहीं भौतिक स्तर पर ऐसी परिस्थितियाँ और व्यवस्थाएँ विकसित होती गयीं तथा उन्होंने ऐसी चिन्तन धाराओं को प्रेरित किया जो प्रकारान्तर से मनुष्य की सार्थकता और मूल्यवत्ता में अविश्वास करती गयीं। बहुधा ऐसी विचारधाराएँ नाम के लिए मानवतावाद के साथ विशिष्ट विशेषण जोड़कर उसका प्रश्रय लेती रही हैं। किन्तु: मूलत: वे मानव की गरिमा को कुण्ठित करने में सहायक हुई हैं और मानव का अवमूल्यन करती गयी हैं।
सांस्कृतिक संकट या मानवीय तत्त्व के विघटन की जो बात बहुधा उठाई जाती रही है, उसका तात्पर्य यही है कि वर्तमान युग में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं जिसमें अपनी नियति के, इतिहास-निर्माण के सूत्र मनुष्य के हाथों से छूटे हुए लगते हैं-मनुष्य दिनोंदिन निरर्थकता की ओर अग्रसर होता प्रतीत होता है। यह संकट केवल आर्थिक या राजनीतिक संकट नहीं है वरन् जीवन के सभी पक्षों में समान रूप से प्रतिफलित हो रहा है। यह संकट केवल पश्चिम या पूर्व का नहीं है वरन् समस्त संसार में विभिन्न धरातलों पर विभिन्न रुपों में प्रकट हो रहा है।
प्रस्तुत पुस्तक में साहित्य को इसी वर्तमान मानवीय संकट के सन्दर्भ में देखने की और जाँचने की चेष्टा की गयी है। साहित्य मनुष्य का ही कृतित्व है और मानवीय चेतना के बहुविध प्रयत्नरों (Responses) में से एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रत्युत्तर है। इसलिए हम आधुनिक साहित्य के बहुत-से पक्षों को या आयामों को केवल तभी बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं जब हम उन्हें मानव-मूल्यों के इस व्यापक संकट के सन्दर्भ में देखने की चेष्टा करें।
अभी तक हिन्दी साहित्य के तमाम अध्ययनों में दो दृष्टिकोण लिये जाते रहे हैं। या तो हिन्दी साहित्य को अपने में एक संपूर्ण वृत्त मानकर उसका अध्ययन इस तरह किया जाता था जैसे वह शेष सभी बाहरी सन्दर्भों से विच्छिन्न हो। या इसका स्वरूप था कि उस पर बाहरी शक्तियों और धाराओं के प्रभावों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाता रहा है गोया वह केवल निष्क्रिय तत्त्व है जिसे दूसरे केवल प्रभावित कर सकते हैं। किन्तु वह केवल दूसरे साहित्यों से ‘प्रभावित’ ही नहीं हुआ है वरन् विश्व इतिहास की समस्त प्रक्रिया में स्वयं एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में उसने संकट का सामना किया है; नये मूल्यों के विकास की भूमिका प्रस्तुत की है और तमाम साहित्यों के बीच वह केवल दूसरों से प्रभावित होने की वस्तु ही नहीं रही है वरन् उन तमाम आधुनिक परिस्थितियों के बीच उसका अपना सहज स्वाभाविक उन्मेष हुआ है।
प्रस्तुत पुस्तक में इसीलिए पहले व्यापक सांस्कृतिक संकट का सर्वेक्षण किया गया है और तब उसके सन्दर्भ में हिन्दी साहित्य की बात की गई है। हिन्दी के प्रसंग में लेखक ने छायावाद और प्रगतिवाद दोनों के प्रति असंतोष व्यक्त किया है क्योंकि उसके विचार में एक ने मूल समस्या का सामना ही नहीं किया और दूसरे ने समस्या को गलत परिप्रेक्ष्य में उठाकर उलझनें बढ़ा दीं। अपनी सहमति-असहमति को लेखक ने स्पष्ट और बलपूर्वक रखने की चेष्टा की है क्योंकि उसका विश्वास है कि चिन्तन के क्षेत्र में यह आवश्यक भी है और उपयोगी भी।
यह पुस्तक लगभग तीन वर्ष पूर्व ही पाठकों के सामने आ जानी चाहिए थी, लेकिन परिस्थितियोंवश इसके प्रकाशन में विलम्ब होता गया। इसके लेखन के दौरान सर्वश्री लक्ष्मीकान्त वर्मा, डॉ. रघुवंश, फादर आई.ए.एक्स्ट्रास, विजयदेव नारायण साही तथा डॉ.रामस्वरूप चतुर्वेदी से अक्सर विचार-विनिमय होता रहा है जिससे मेरे चिन्तन को बहुत प्रेरणा मिली है। मैं उन सबों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।
ज्यों-ज्यों हम आधुनिक युग में प्रवेश करते गये त्यों-त्यों इस मानवोपरि सत्ता का अवमूल्यन होता गया। मनुष्य की गरिमा का नये स्तर पर उदय हुआ और माना जाने लगा कि मनुष्य अपने में स्वत: सार्थक और मूल्यवान् है-वह आन्तरिक शक्तियों से संपन्न, चेतन-स्तर पर अपनी नियति के निर्माण के लिए स्वत: निर्णय लेने वाला प्राणी है। सृष्टि के केन्द्र में मनुष्य है। यह भावना बीच-बीच में मध्यकाल के साधकों या सन्तों में भी कभी-कभी उदित हुई थी, किन्तु आधुनिक युग के पहले यह कभी सर्वमान्य नहीं हो पायी थी।
लेकिन जहाँ तक एक ओर सिद्धांतों के स्तर पर मनुष्य की सार्वभौमिक सर्वोपरि सत्ता स्थापित हुई, वहीं भौतिक स्तर पर ऐसी परिस्थितियाँ और व्यवस्थाएँ विकसित होती गयीं तथा उन्होंने ऐसी चिन्तन धाराओं को प्रेरित किया जो प्रकारान्तर से मनुष्य की सार्थकता और मूल्यवत्ता में अविश्वास करती गयीं। बहुधा ऐसी विचारधाराएँ नाम के लिए मानवतावाद के साथ विशिष्ट विशेषण जोड़कर उसका प्रश्रय लेती रही हैं। किन्तु: मूलत: वे मानव की गरिमा को कुण्ठित करने में सहायक हुई हैं और मानव का अवमूल्यन करती गयी हैं।
सांस्कृतिक संकट या मानवीय तत्त्व के विघटन की जो बात बहुधा उठाई जाती रही है, उसका तात्पर्य यही है कि वर्तमान युग में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं जिसमें अपनी नियति के, इतिहास-निर्माण के सूत्र मनुष्य के हाथों से छूटे हुए लगते हैं-मनुष्य दिनोंदिन निरर्थकता की ओर अग्रसर होता प्रतीत होता है। यह संकट केवल आर्थिक या राजनीतिक संकट नहीं है वरन् जीवन के सभी पक्षों में समान रूप से प्रतिफलित हो रहा है। यह संकट केवल पश्चिम या पूर्व का नहीं है वरन् समस्त संसार में विभिन्न धरातलों पर विभिन्न रुपों में प्रकट हो रहा है।
प्रस्तुत पुस्तक में साहित्य को इसी वर्तमान मानवीय संकट के सन्दर्भ में देखने की और जाँचने की चेष्टा की गयी है। साहित्य मनुष्य का ही कृतित्व है और मानवीय चेतना के बहुविध प्रयत्नरों (Responses) में से एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रत्युत्तर है। इसलिए हम आधुनिक साहित्य के बहुत-से पक्षों को या आयामों को केवल तभी बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं जब हम उन्हें मानव-मूल्यों के इस व्यापक संकट के सन्दर्भ में देखने की चेष्टा करें।
अभी तक हिन्दी साहित्य के तमाम अध्ययनों में दो दृष्टिकोण लिये जाते रहे हैं। या तो हिन्दी साहित्य को अपने में एक संपूर्ण वृत्त मानकर उसका अध्ययन इस तरह किया जाता था जैसे वह शेष सभी बाहरी सन्दर्भों से विच्छिन्न हो। या इसका स्वरूप था कि उस पर बाहरी शक्तियों और धाराओं के प्रभावों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाता रहा है गोया वह केवल निष्क्रिय तत्त्व है जिसे दूसरे केवल प्रभावित कर सकते हैं। किन्तु वह केवल दूसरे साहित्यों से ‘प्रभावित’ ही नहीं हुआ है वरन् विश्व इतिहास की समस्त प्रक्रिया में स्वयं एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में उसने संकट का सामना किया है; नये मूल्यों के विकास की भूमिका प्रस्तुत की है और तमाम साहित्यों के बीच वह केवल दूसरों से प्रभावित होने की वस्तु ही नहीं रही है वरन् उन तमाम आधुनिक परिस्थितियों के बीच उसका अपना सहज स्वाभाविक उन्मेष हुआ है।
प्रस्तुत पुस्तक में इसीलिए पहले व्यापक सांस्कृतिक संकट का सर्वेक्षण किया गया है और तब उसके सन्दर्भ में हिन्दी साहित्य की बात की गई है। हिन्दी के प्रसंग में लेखक ने छायावाद और प्रगतिवाद दोनों के प्रति असंतोष व्यक्त किया है क्योंकि उसके विचार में एक ने मूल समस्या का सामना ही नहीं किया और दूसरे ने समस्या को गलत परिप्रेक्ष्य में उठाकर उलझनें बढ़ा दीं। अपनी सहमति-असहमति को लेखक ने स्पष्ट और बलपूर्वक रखने की चेष्टा की है क्योंकि उसका विश्वास है कि चिन्तन के क्षेत्र में यह आवश्यक भी है और उपयोगी भी।
यह पुस्तक लगभग तीन वर्ष पूर्व ही पाठकों के सामने आ जानी चाहिए थी, लेकिन परिस्थितियोंवश इसके प्रकाशन में विलम्ब होता गया। इसके लेखन के दौरान सर्वश्री लक्ष्मीकान्त वर्मा, डॉ. रघुवंश, फादर आई.ए.एक्स्ट्रास, विजयदेव नारायण साही तथा डॉ.रामस्वरूप चतुर्वेदी से अक्सर विचार-विनिमय होता रहा है जिससे मेरे चिन्तन को बहुत प्रेरणा मिली है। मैं उन सबों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।
बुधवार, 9 मार्च
धर्मवीर भारती
अन्तरात्मा के ध्वंसावशेष
‘‘अपने हृदय पर कीलों से ठुकी हुई जैसे सलीब पर चोर
मैं लटक रही हूँ बीचोंबीच-जीसस् के और उस खाई के-जहाँ इस संसार
का अन्त हो गया है !.....
..............................................................
जीवित अन्धे और द्रष्टा मुर्दे एक साथ पड़े हुए हैं
जैसे प्रेमी.....और न अब नफरत रही है
और न प्रेम है। लुप्त हो गया है मनुष्य का हृदय।’’
मैं लटक रही हूँ बीचोंबीच-जीसस् के और उस खाई के-जहाँ इस संसार
का अन्त हो गया है !.....
..............................................................
जीवित अन्धे और द्रष्टा मुर्दे एक साथ पड़े हुए हैं
जैसे प्रेमी.....और न अब नफरत रही है
और न प्रेम है। लुप्त हो गया है मनुष्य का हृदय।’’
(एडिथ सिटवेल : ‘अणुबम पर तीन कविताएँ’)
एडिथ सिटवेल की ये पंक्तियाँ सन् 1947 में लिखी गयी थीं और इसका शीर्षक था ‘नये सूर्योदय का मरसिया’। लगभग समस्त पाश्चात्य साहित्य में, द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद जो साहित्य आया उसमें उसी विषाद, दुश्चिन्ता बेचैनी की प्रतिध्वनि मिलती है जो इन पंक्तियों में हैं पश्चिम ने यह अनुभव कर लिया था कि वह एक ऐसे बिन्दु पर पहुँच गया है जिसके आगे अँधेरा है, अनिश्चय है, दिग्भ्रम है। यह सिटवेल नहीं बल्कि यूरोप का मानस बोल रहा था जो ‘‘लटक रहा था बीचोंबीच-जीसस् के और उस खाई के जहाँ इस संसार का अन्त हो गया है।’’ .....और जहाँ भले-बुरे की दीवार टूट गयी है। जहाँ शब्द कुछ और हैं, आचार कुछ और हैं; कर्म कुछ है, परिणाम दूसरा। पश्चिम की समस्त व्यवस्था तूफान में पड़े हुए ऐसे जहाज की तरह हो गयी है जिसके पाल फट चुके हैं, पतवारें टूट चुकी हैं, माझी बेकाम हो चुके हैं। उत्ताल लहरों पर निरुद्देश्य डोलता हुआ एक विशाल पोत। द्वितीय महायुद्ध के बाद जिस अस्तित्ववादी विचारधारा का आकस्मिक प्रसार पश्चिम में हुआ, उसमें बार-बार जो प्रतीक प्रयुक्त हुआ है, वह इसी तूफान में ध्वस्त जहाज का !
पिछली शताब्दी में ही यूरोपीय-साहित्य में ध्वस्त होती हुई इस अन्तरात्मा का स्पष्ट आभास मिलने लगा था। विशेषतया डास्टावस्की की कथाकृतियों में मानवीय अन्तरात्मा का जो विराट् मानचित्र प्रस्तुत किया था वह एक विशाल पैमाने पर घटित होते हुए विघटन का सूचक था, एक बहुत बड़े आसन्न संकट का द्योतक था। पश्चिम के कथा-साहित्य और नाटकों में कर्मठ नायकों का स्थान दिनोंदिन ऐसे नायक ले रहे थे जो अन्तर्द्वन्द्व से ग्रस्त थे, निष्क्रिय थे। एक अजीब से दिग्भ्रम और जड़ मूर्छना के शिकार थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे इतिहास के सूत्र बुरी तरह उलझ गये थे। उनके बीच में अन्तरात्मा का कोई जोर नहीं चल पाता था। इतिहास से उसकी कोई संगति नहीं बैठ पाती थी। जैविक विकास के नियमों के अनुसार जैसे जिन पक्षियों के पंख काम नहीं आते हैं, वे दिनोंदिन उड़ने की शक्ति खोते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, नाममात्र के रह जाते हैं, उसी प्रकार दिनों दिन मानवीय अन्तरात्मा सर्वथा निश्शक्त होकर विलुप्त होती जा रही थी। या यदि रह भी गयी थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यह अन्तरात्मा केवल कुछ अव्यावहारिक अन्तर्मुखी स्वप्नदर्शियों का अनावश्यक मानसिक उद्वेग बनकर रह गयी है, जिसका बाह्य यथार्थ से कोई मेल नहीं पैठ पाता।
यह स्थिति धीरे-धीरे कैसे विकसित हुई और क्रमश: किन अवस्थाओं से गुजरकर पाश्चात्य-चेतना इस बिन्दु तक पहुँची इसका एक बहुत लम्बा इतिहास है किन्तु यहाँ पर केवल इतना संकेत कर देना यथेष्ट होगा कि विज्ञान के उदय ने पुरानी मान्यताओं के समक्ष गहरे प्रश्न-चिह्न लगा दिये थे और मनुष्य पहले जिन धर्म-ग्रन्थों में प्रणीत नियमों या आचार-विधानों को अन्तरात्मा की आधार-भूमि मानता था, वे धीरे-धीरे निरर्थक सिद्ध हो चुके थे। मानवतावाद के उदयकाल में ईश्वर जैसा किसी मानवोपरि सत्ता या उसके प्रतिनिधि धर्माचार्यों को नैतिक मूल्यों का अधिनायक न मानकर मनुष्य को ही इन मूल्यों का विधायक मानने की प्रवृत्ति विकसित होने लगी थी।
इसी समय पहली बार यह स्पष्ट हो सका था कि ‘अन्तकात्मा’ मानवीय अन्तर में स्थित कोई दैव या अतिप्राकृतिक शक्ति न होकर वस्तुत: मानवीय गरिमा के प्रति हमारा संवेदनशीलता का ही दूसरा रूप है और मनुष्य के गौरव को प्रतिष्ठित करने और उसकी निरन्तर रक्षा करने के प्रति हमारी जागरूकता ही हमारी जाग्रत अन्तरात्मा काल प्रमाण है। उसी समय पहली बार यह भू स्वीकार किया गया था कि पुराने मूल्य अब मिथ्या पड़ने लगे हैं। ऐसी श्रद्धा और आस्था द्वारा व्यक्त हो पर समाज के वैषम्य को विधि का विधान मानकर स्वीकार कर ले-इस प्रकार की श्रद्धा और करुणा अमानवीय वृत्तियों को जन्म देते हैं। वे मानवीय गौरव को प्रतिष्ठित करने की बजाय उसको विकलांग बनाते हैं उसी समय पहली बार यह भी स्पष्ट होने लगा कि विवेक अन्तरात्मा के सहायक तत्त्वों में सम्भवत: सबसे प्रमुख और सबसे विश्वसनीय है। मानवीय गौरव के अर्थ यह हैं कि मनुष्य को स्वतन्त्र, सचेत, दायित्वयुक्त माना जाये जो अपनी नियति, अपने इतिहास का निर्माता हो सकता है। इसके लिए उसके विवेक और मनोबल को सर्वोपरि और अपराजेय माना जाय।
कहा जाता है कि मृत्यु के कुछ पहले न केवल व्यक्तियों वरन् संस्कृतियों को भी एक विचित्र-सी दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वे जीवन के आरपार देखने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानववाद के उदयकाल में यूरोप को कुछ वैसी ही दृष्टि प्राप्त हो गयी थी। दीपक बुझने से पहले जैसे अन्तिम लौ फेंक रहा था और उसके बाद ही जैसे उसकी शिखा काँपने और टिमटिमाने लगी। एक ओर यह नवोपलब्ध दृष्टि और दूसरी ओर अकस्मात् पूरी सांस्कृतिक व्यवस्था का सहसा चरमरा उठना।
यह नहीं कि उसमें उत्साह की कमी थी। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा ही था जो सन्निपातग्रस्त रोगी की भाँति बेहद आवेश में था, उत्साह में था, अदम्य आशावादी था, जो यूरोपीय संस्कृति की आन्तरिक असंगतियों और उसके आसन्न विनाश को केवल निराशावादियों का प्रलाप समझते हुए यूरोप की विश्वविजय के स्वप्न देख रहा था, जैसे किपलिंग; या इस समस्त उथल-पुथल को किसी महामानव के अवतरण भी भूमिका मान रहा था, जैसे नीत्शे ! यथार्थ की घोर उपेक्षा कर प्रवंचना के कल्पित स्वप्न जगत् में निरन्तर निवास करने वालों के ऐसे ही आशावाद को देखकर किसी विचारक ने यह कहा होगा कि ‘आशावादी का उपयुक्त आश्रयस्थल है-पागलखाना !
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book