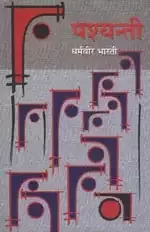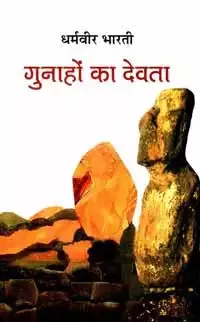|
लेख-निबंध >> पश्यन्ती पश्यन्तीधर्मवीर भारती
|
185 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है धर्मवीर भारती का एक बहुआयामी निबन्ध संग्रह...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
पश्यन्ती के निबन्धों में धर्मवीर भारती की एक ऐसी बहुआयामी
साहित्य-दृष्टि मिलेगी जो इतिहास की हवाओं की हर हलकी से हलकी हिलोर पर
संवेदनशील मुलायम पीपल पाल की तरह कांप उठे। ग्रीक वीणा की तरह झंकार भी
दे, और खुले हुए पाल की तरह तनकर तेज हवाओं को आत्मस्य कर, तूफानों को
चीरने का साहस-पथ भी निर्दिष्टि करे।
भारती जी ने समय-समय पर अनेक विषयों पर लिखा है और जब भी लिखा वह अत्यंत विचारोत्तेजक रहा है। इसीलिए उसकी व्यापक चर्चा भी हुई है। ‘पश्यन्ती’ उनके ऐसे ही कुछ निबन्धों का संकलन है। इन निबन्धों में मुखर व्यापक अध्ययन, प्रखर विश्लेषण, गहन चिंतन, पैनी ज्वलन्त शैली और मौलिक विवेचन का साहस सब मिलकर एक अनूठे रस का संचार करते हैं।
प्रस्तुत है इस बहुचर्चित कृति का एक नया संस्करण।
‘‘यह एक पहेली-सी है। विवेक एक ओर खुलाव चहता है, आजाद रहना चहता है, दूसरी ओर अपने को बद्ध करता है ताकि एक मूर्त ऐतिहासिक क्षम में एक निश्चय तक पहुँच सके...सांस्कृतिक स्वाधीनता तभी बनी रह सकती है जब विवेक युक्त स्वतन्त्र मानस से निर्णीत कार्य सांस्कृतिक अभियानों को उचित दिशाएँ देते रहें। आन्तरिक स्वातन्त्र्य की अनिवार्य शर्त है-दायित्व-भावना।
दायित्वपूर्ण सांस्कृतिक स्वातन्त्र्य का एक ही बदल है-सांस्कृतिक अराजकता। मनुष्य के लिए स्वातन्त्र्य आवश्यक है लेकिन कोई व्यक्ति या कोई सत्ता उसे दायित्वपूर्ण होने के लिये मजबूर नहीं कर सकते। इसीलिए स्वयं स्वातन्त्र्य जब वह दायित्वहीन होकर असफल होता है तो गुलामी को जन्म देता है।...वे लोग जो पूर्ण अविवेक के जादू के मदारी है।–वे आक्रामकता और हिंसा उठाते हैं-बिना जाने हुए कि क्यों और कैसे ?’’
भारती जी ने समय-समय पर अनेक विषयों पर लिखा है और जब भी लिखा वह अत्यंत विचारोत्तेजक रहा है। इसीलिए उसकी व्यापक चर्चा भी हुई है। ‘पश्यन्ती’ उनके ऐसे ही कुछ निबन्धों का संकलन है। इन निबन्धों में मुखर व्यापक अध्ययन, प्रखर विश्लेषण, गहन चिंतन, पैनी ज्वलन्त शैली और मौलिक विवेचन का साहस सब मिलकर एक अनूठे रस का संचार करते हैं।
प्रस्तुत है इस बहुचर्चित कृति का एक नया संस्करण।
‘‘यह एक पहेली-सी है। विवेक एक ओर खुलाव चहता है, आजाद रहना चहता है, दूसरी ओर अपने को बद्ध करता है ताकि एक मूर्त ऐतिहासिक क्षम में एक निश्चय तक पहुँच सके...सांस्कृतिक स्वाधीनता तभी बनी रह सकती है जब विवेक युक्त स्वतन्त्र मानस से निर्णीत कार्य सांस्कृतिक अभियानों को उचित दिशाएँ देते रहें। आन्तरिक स्वातन्त्र्य की अनिवार्य शर्त है-दायित्व-भावना।
दायित्वपूर्ण सांस्कृतिक स्वातन्त्र्य का एक ही बदल है-सांस्कृतिक अराजकता। मनुष्य के लिए स्वातन्त्र्य आवश्यक है लेकिन कोई व्यक्ति या कोई सत्ता उसे दायित्वपूर्ण होने के लिये मजबूर नहीं कर सकते। इसीलिए स्वयं स्वातन्त्र्य जब वह दायित्वहीन होकर असफल होता है तो गुलामी को जन्म देता है।...वे लोग जो पूर्ण अविवेक के जादू के मदारी है।–वे आक्रामकता और हिंसा उठाते हैं-बिना जाने हुए कि क्यों और कैसे ?’’
नवलेखनः माध्यम मैं
(कुछ स्नैपशॉट्स)
मैंने अमुक कृति क्यों लिखी ? कब लिखी ? उसके द्वारा नव लेखन का कौन-सा
पक्ष उभरा, क्या उसने कोई मान, स्थापित किये ?-ये सवाल दरपेश हैं।
और मेरा मन है कि पुरानी यादों में डूब जाने को आतुर है। उसे इतनी भी ताब नहीं कि सवालों का मुख्तसर-सा जवाब देने का शिष्टाचार तो निभा दे ! सवालों को साथ-साथ लिये-दिये वह यादों में डुबकी लगा जाता है...
(1)
और मेरा मन है कि पुरानी यादों में डूब जाने को आतुर है। उसे इतनी भी ताब नहीं कि सवालों का मुख्तसर-सा जवाब देने का शिष्टाचार तो निभा दे ! सवालों को साथ-साथ लिये-दिये वह यादों में डुबकी लगा जाता है...
(1)
‘‘सम्मुख होकर जो भी आया है और गया भी है
बाँधा है उसने मुझको हर बार और नया भी है
.......................................................................................
दुनिया के मेले में केवल बच्चा हूँ !’’
बाँधा है उसने मुझको हर बार और नया भी है
.......................................................................................
दुनिया के मेले में केवल बच्चा हूँ !’’
अजित कुमार
...चारों तरफ मेला लगा है। भीड़-भाड़,
खरीद-फरोख्त,
आवा-जाही। झूलों की चरर-मरर, सर्कस का भोंपू, आरती के घण्टे। मैंने
मनिहारिन का वह रंगीन काँच का खिलौना मोल ले लिया है और उसे हर तरफ से खोल
डाला है। कहाँ गया वह खूबसूरत तिलिस्म ? काँच की दो-तीन नलियाँ और कटोरी
में सादा पानी ! मैं हक्का-बक्का हूँ और लज्जित। मनिहारिन हँस रही है जीजी
हँस रही है दूकान पर खड़े दूसरे बच्चे और बड़े हँस रहे हैं। चारों ओर की
विद्रूप-भरी हँसी से आहत होकर मेरा शिशुमन घबरा गया है, आँखें छलछला आयी
हैं और बस यही इच्छा हो रही है कि जीजी मेरे हाथ छोड़ दें और मैं भागता
हुआ जाऊँ और सीधे जमुना में डूब मरूँ। मैंने उस काँच के तिलिस्म का
अन्दरूनी क्या और कहा देखना चाहा था और हाथ लगे सिर्फ काँच के टुकड़े,
पानी और हँसी के ठहाके !
मेला कातिक का था, तो हर साल जमुना किनारे लगता था। अब भी लगता होगा। रेशम, ऊनी कपड़े, साड़ियाँ, बर्तन, चूड़ियाँ, सीपी के बटन, सिन्दूर, सुई के पत्ते पत्थर की कूँड़ियाँ, रँगे हुए बेलन, क्या नहीं मिलता था वहाँ ! माँ आर्यसमाजी हैं। इन मेलों-ठेलों ने देश को नाश किया, अतः उन्हें इसमें दिलचस्पी नहीं। बगल वाले घर में जीजी का मैं लाड़ला था। उनके ठाकुर जी के लिए स्कूल के अहाते से कनेर और मधुमालती के फूल लाने से लेकर दोपहर को चिल्लाकर राधेश्याम की रामायण गाना मेरा रोज का कार्यक्रम था। फलस्वरूप हर छठ पर छोटी-छोटी कुल्हियों में भुने चने, मकाई, मटर भरने में जन्माष्टमी पर पंजीरी, पंचामृत बनाने में और कातिक में मेले से सालभर की खरीद-फरोख्त करने में मैं उनका सलाहकार और छोटा सिपाही था।
इस बार मेले में मनिहार की दूकान की चर्चा बहुत जोर में थी। फतेहपुर वाली चाची ने मेले से लौटकर बताया, ‘‘हाय मैया, ऐसा बढ़िया फब्वारा है कि बीस रंग का पानी ओमें कुलेल करता है, और छुवै की जरूरत नैं, चाभी लगाय देव और फब्वारा आपै-आप चलत रहत है।’’ जब ऐसी चीज आयी है तो जीजी अपने लाड़ले छोटे सिपाही को कैसे न दिलाएँ ! दो रूपया मुझे दिया गया और मैं मेले में गया। चूड़ियों की दूकान। कुछ चूड़ियाँ अन्दर से खोखली होती हैं। बहुत से रंगों की ऐसी तमाम चूड़ियों को जोड़-जोड़कर एक गोरखधन्धा सा बनाया गया था। ऊपर नीचे दो टीन के बर्तन थे, जिनका पानी इस गोरखधन्धा से होकर गुजरता था। लगता था, हजारों रंग काँच की उन नालियों में से बेतहाशा पगलाये हुए दौड़ रहे हैं। एक-दूसरे की आभा लेकर नये-नये रंग बन रहे हैं। और कातिक के सवेरे की हल्की धूप में उन रंगों की छाया-किरणों के ऊपर-ऊपर साथ-साथ दौड़ रही हैं। जिसने देखा, मन्त्रमुग्ध रह गया। खिलौने का दाम पाँच रुपये था। जीजी ने मेरे मुँह पर उत्सुकता देखी, बगल वाले जान-पहचान के खत्री बिसाती से तीन रुपये तुरन्त उधार लिये और खिलौना मेरा हो गया।
इस होनहार बिरवान के पात चीकने तो नहीं रहे, न आज हैं पर शायद नव लेखन के किसी भावी व्याख्याकार की आत्मा मेरी काया में प्रवेश कर गयी होगी तभी वह तिलिस्म हाथ में आ जाने के बाद नवलेखन का बौद्धिक, वैज्ञानिक और विश्लेषक आधुनिक मिजाज मुझमें जागा। बौद्धिक मिजाज ने जनाना चाहा कि इतने रंग इसमें कहां से आते हैं। वैज्ञानिक मिजाज ने निश्चय कर लिया कि जो बात मणिहार जैसा महामानव कर सकता है, वह मुझ जैसा लघुमानव क्यों न कर लेगा ! विश्लेषक मिजाज ने पाँच रुपये दिये और पानी के बर्तन और काँच की नली के बीट के रबड़ ट्यूब को निकाल दिया। पानी नीचे गिर गया। उसके बाद मैंने पुनसृर्जन शुरू किया मगर पानी नहीं आया तो नहीं आया ! भीड़ में से दो-चार ज्ञानियों ने आजमूदा नुस्खे बताये मगर बात बिगड़ती गयी। उनके बाद पहले मनिहारिन हँसी और फिर भीड़। मैं लौटा तो खिलौना जीजी की डोलची में था, मगर मेरे गाल पर आँसू की बड़ी-बड़ी लकीरें बन गयी थीं और हर दस कदम पर एक हिचकी आ ही जाती थी।
मेला आज भी लगा है। लेकिन एक साधारण करामात के खिलौने का विश्लेषण जिससे नहीं हो सका, वह बड़ी सम्पूर्ण कृतियों का ब्यौरेवार विश्लेषण करके रख दे, वैसे गर्व बचपन के साथ चला गया। सिर्फ इतना जानता हूँ कि साधारण शिल्प में भी जाने कितनी चीजें होती हैं जो मिलकर गति का, रंग का, वैविध्य का आभास देती हैं। मगर जो मूल स्रोतस्विनी उस रंग-बिरंगे परिवेश में से बहती है, वह उद्गमस्रोत और अभीष्ट गन्तव्य के किस सापेक्ष सन्तुलन से आती है, बात तो अभी भी धीरे-धीरे जानने के लिए हर अच्छे बुरे में से जी रहा हूँ।
वैसे मेले में आसपास कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने-अपने आजमूदा नुख्से हैं। वे सब कुछ पहले से ही जानते हैं, जानते आये हैं, और जानते रहेंगे। खुद उन्होंने कभी कोई चीज बनायी है या नहीं, नहीं मालूम। कभी-कभी चीज का मूल्य दिया है। जीवन में यह नहीं, यह भी नहीं मालूम। लेकिन उनके आजमूदा नुख्सों की घोषणा बराबर-बराबर सुन पड़ती है। यह उनके आधार पर विश्लेषण करने चले तो उससे बात और बिगड़ती जाती है। बस इतना जानता हूँ कि मैं जितना नहीं जान पाया हूँ, उसके बारे में यह गर्व नहीं है कि वह सब मेरा जाना हुआ है। पर साथ ही साथ न जानने की स्थिति को भगवान की कृपा मानकर बैठ जाऊँ और जानने को, जानने की प्यास को और सारी कोशिशों के बावजूद न जान पाने की आकुलता-भरी तड़प को हेय मानूँ, तिरस्कार योग्य मानूँ, यह भी नहीं है। जीवन के मर्म को पूरी तरह न जानने का का बोध, जानने को चरम आकुल प्यास और उसको जानने की प्रक्रिया में ही अच्छे-बुरे, तीखे और फीके हर रंग में से एकरंग होकर बहते जाने की अथक गति, अभी तक तो यही उपलब्धि है।
यह मिजाज पिछले युग के मिजाज से थोड़ा भिन्न जरूर है। अंग्रेजी का रोमान्टिक कवि जानने को बहुत महत्त्व नहीं देता था उससे प्रभावित पूर्व का छायावादी कवि रहस्य और विस्मय को वरदान मानता था। एक वर्ग ऐसा था, और है जिसके सामने जानना कोई समस्या ही नहीं। वह सब कुछ जानता है। उसके पास हर चीज के नपे-तुले प्रतिमान थे। लेकिन यह कैसे कह दूँ कि ऐसे लोग नवलेखन के पहले ही थे और नवलेखन में नहीं हैं ? इसलिए अधिक से अधिक यह कह सकता हूँ कि यह न जानने का बोध जानने की प्यास जानने की प्रकिया में जीने और जीने की प्रक्रिया में जाननेवाला मिजाज जिन लोगों का है, उनमें मैं अपने को पाता हूँ। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली नहीं होते। वे अधिक से अधिक यह कहकर अपने को सन्तोष दे सकते हैं कि भाग्यशाली न होना ही उनकी ताकत है वे यह भी पाते है कि तमाम चीजों के बीच शायद उनका एक अंश तटस्थ द्रष्टा बना रहता है, संजय की भाँति। और अक्सर राज्य कौरवों का होता है और जिसे शासन-शत्ता के सामने उसे विवरण देना पड़ता है, उसके आँखें नहीं होतीं।
(2)
मेला कातिक का था, तो हर साल जमुना किनारे लगता था। अब भी लगता होगा। रेशम, ऊनी कपड़े, साड़ियाँ, बर्तन, चूड़ियाँ, सीपी के बटन, सिन्दूर, सुई के पत्ते पत्थर की कूँड़ियाँ, रँगे हुए बेलन, क्या नहीं मिलता था वहाँ ! माँ आर्यसमाजी हैं। इन मेलों-ठेलों ने देश को नाश किया, अतः उन्हें इसमें दिलचस्पी नहीं। बगल वाले घर में जीजी का मैं लाड़ला था। उनके ठाकुर जी के लिए स्कूल के अहाते से कनेर और मधुमालती के फूल लाने से लेकर दोपहर को चिल्लाकर राधेश्याम की रामायण गाना मेरा रोज का कार्यक्रम था। फलस्वरूप हर छठ पर छोटी-छोटी कुल्हियों में भुने चने, मकाई, मटर भरने में जन्माष्टमी पर पंजीरी, पंचामृत बनाने में और कातिक में मेले से सालभर की खरीद-फरोख्त करने में मैं उनका सलाहकार और छोटा सिपाही था।
इस बार मेले में मनिहार की दूकान की चर्चा बहुत जोर में थी। फतेहपुर वाली चाची ने मेले से लौटकर बताया, ‘‘हाय मैया, ऐसा बढ़िया फब्वारा है कि बीस रंग का पानी ओमें कुलेल करता है, और छुवै की जरूरत नैं, चाभी लगाय देव और फब्वारा आपै-आप चलत रहत है।’’ जब ऐसी चीज आयी है तो जीजी अपने लाड़ले छोटे सिपाही को कैसे न दिलाएँ ! दो रूपया मुझे दिया गया और मैं मेले में गया। चूड़ियों की दूकान। कुछ चूड़ियाँ अन्दर से खोखली होती हैं। बहुत से रंगों की ऐसी तमाम चूड़ियों को जोड़-जोड़कर एक गोरखधन्धा सा बनाया गया था। ऊपर नीचे दो टीन के बर्तन थे, जिनका पानी इस गोरखधन्धा से होकर गुजरता था। लगता था, हजारों रंग काँच की उन नालियों में से बेतहाशा पगलाये हुए दौड़ रहे हैं। एक-दूसरे की आभा लेकर नये-नये रंग बन रहे हैं। और कातिक के सवेरे की हल्की धूप में उन रंगों की छाया-किरणों के ऊपर-ऊपर साथ-साथ दौड़ रही हैं। जिसने देखा, मन्त्रमुग्ध रह गया। खिलौने का दाम पाँच रुपये था। जीजी ने मेरे मुँह पर उत्सुकता देखी, बगल वाले जान-पहचान के खत्री बिसाती से तीन रुपये तुरन्त उधार लिये और खिलौना मेरा हो गया।
इस होनहार बिरवान के पात चीकने तो नहीं रहे, न आज हैं पर शायद नव लेखन के किसी भावी व्याख्याकार की आत्मा मेरी काया में प्रवेश कर गयी होगी तभी वह तिलिस्म हाथ में आ जाने के बाद नवलेखन का बौद्धिक, वैज्ञानिक और विश्लेषक आधुनिक मिजाज मुझमें जागा। बौद्धिक मिजाज ने जनाना चाहा कि इतने रंग इसमें कहां से आते हैं। वैज्ञानिक मिजाज ने निश्चय कर लिया कि जो बात मणिहार जैसा महामानव कर सकता है, वह मुझ जैसा लघुमानव क्यों न कर लेगा ! विश्लेषक मिजाज ने पाँच रुपये दिये और पानी के बर्तन और काँच की नली के बीट के रबड़ ट्यूब को निकाल दिया। पानी नीचे गिर गया। उसके बाद मैंने पुनसृर्जन शुरू किया मगर पानी नहीं आया तो नहीं आया ! भीड़ में से दो-चार ज्ञानियों ने आजमूदा नुस्खे बताये मगर बात बिगड़ती गयी। उनके बाद पहले मनिहारिन हँसी और फिर भीड़। मैं लौटा तो खिलौना जीजी की डोलची में था, मगर मेरे गाल पर आँसू की बड़ी-बड़ी लकीरें बन गयी थीं और हर दस कदम पर एक हिचकी आ ही जाती थी।
मेला आज भी लगा है। लेकिन एक साधारण करामात के खिलौने का विश्लेषण जिससे नहीं हो सका, वह बड़ी सम्पूर्ण कृतियों का ब्यौरेवार विश्लेषण करके रख दे, वैसे गर्व बचपन के साथ चला गया। सिर्फ इतना जानता हूँ कि साधारण शिल्प में भी जाने कितनी चीजें होती हैं जो मिलकर गति का, रंग का, वैविध्य का आभास देती हैं। मगर जो मूल स्रोतस्विनी उस रंग-बिरंगे परिवेश में से बहती है, वह उद्गमस्रोत और अभीष्ट गन्तव्य के किस सापेक्ष सन्तुलन से आती है, बात तो अभी भी धीरे-धीरे जानने के लिए हर अच्छे बुरे में से जी रहा हूँ।
वैसे मेले में आसपास कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने-अपने आजमूदा नुख्से हैं। वे सब कुछ पहले से ही जानते हैं, जानते आये हैं, और जानते रहेंगे। खुद उन्होंने कभी कोई चीज बनायी है या नहीं, नहीं मालूम। कभी-कभी चीज का मूल्य दिया है। जीवन में यह नहीं, यह भी नहीं मालूम। लेकिन उनके आजमूदा नुख्सों की घोषणा बराबर-बराबर सुन पड़ती है। यह उनके आधार पर विश्लेषण करने चले तो उससे बात और बिगड़ती जाती है। बस इतना जानता हूँ कि मैं जितना नहीं जान पाया हूँ, उसके बारे में यह गर्व नहीं है कि वह सब मेरा जाना हुआ है। पर साथ ही साथ न जानने की स्थिति को भगवान की कृपा मानकर बैठ जाऊँ और जानने को, जानने की प्यास को और सारी कोशिशों के बावजूद न जान पाने की आकुलता-भरी तड़प को हेय मानूँ, तिरस्कार योग्य मानूँ, यह भी नहीं है। जीवन के मर्म को पूरी तरह न जानने का का बोध, जानने को चरम आकुल प्यास और उसको जानने की प्रक्रिया में ही अच्छे-बुरे, तीखे और फीके हर रंग में से एकरंग होकर बहते जाने की अथक गति, अभी तक तो यही उपलब्धि है।
यह मिजाज पिछले युग के मिजाज से थोड़ा भिन्न जरूर है। अंग्रेजी का रोमान्टिक कवि जानने को बहुत महत्त्व नहीं देता था उससे प्रभावित पूर्व का छायावादी कवि रहस्य और विस्मय को वरदान मानता था। एक वर्ग ऐसा था, और है जिसके सामने जानना कोई समस्या ही नहीं। वह सब कुछ जानता है। उसके पास हर चीज के नपे-तुले प्रतिमान थे। लेकिन यह कैसे कह दूँ कि ऐसे लोग नवलेखन के पहले ही थे और नवलेखन में नहीं हैं ? इसलिए अधिक से अधिक यह कह सकता हूँ कि यह न जानने का बोध जानने की प्यास जानने की प्रकिया में जीने और जीने की प्रक्रिया में जाननेवाला मिजाज जिन लोगों का है, उनमें मैं अपने को पाता हूँ। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली नहीं होते। वे अधिक से अधिक यह कहकर अपने को सन्तोष दे सकते हैं कि भाग्यशाली न होना ही उनकी ताकत है वे यह भी पाते है कि तमाम चीजों के बीच शायद उनका एक अंश तटस्थ द्रष्टा बना रहता है, संजय की भाँति। और अक्सर राज्य कौरवों का होता है और जिसे शासन-शत्ता के सामने उसे विवरण देना पड़ता है, उसके आँखें नहीं होतीं।
(2)
‘लो मैं वापिस लौटता हूँ
पर, अब जानता हूँ मेरे पीछे
जहां ढाल और पेड़ों का अंत है
एक गुनगुनाती नदी और
एक हंसता हुआ पुल है।
पर, अब जानता हूँ मेरे पीछे
जहां ढाल और पेड़ों का अंत है
एक गुनगुनाती नदी और
एक हंसता हुआ पुल है।
विपिन अग्रवाल
संजय की दृष्टि सिर्फ दिशाओं के वेध कर देखती थी। लेकिन दिक् (स्पेस) के
अतिरिक्त एक दूसरी महत्त्वपूर्ण चीज है काल का समय प्रवाह। हम, हमारी
जिन्दगी जो है वह पहले नहीं थी, जो पहले थी वह अब नहीं है। इतना जानना
बहुत ज्यादा उलझन पैदा नहीं कर सकता; अधिक से अधिक यह गलत या सही धारणा
पैदा करता है कि यह सब माया से उत्पन्न भ्रान्तियाँ हैं और उनसे तटस्थ
होकर मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है। लेकिन जब साक्षात्कार यह होता है कि
जो पहले कभी था वह वहीं पर अब भी है जो आज है उसमें भी उसकी टीस और कसक
निरन्तर विद्यमान है और जो आज है वह उससे बिल्कुल पृथक् है लेकिन कहीं पर
बीज रूप में सही, उसी में विद्यमान था, तो वहीं से संजय की आधुनिक जटिल
समस्या प्रारम्भ होती है। आज संजय को सिर्फ दिशाओं की दूरी नहीं पार करनी
पड़ती, वरन् काल के अजस्र में पैठकर कभी उसे देखना पड़ता है जो आज बीज रूप
में है और कल आ सकता है, कभी उसे पीछे लौटना पड़ता है। जहाँ वह सब था और
नहीं है और न होते हुए भी अपनी जगह बदस्तूर कायम है। आज का संजय बहुत बड़ी
उलझन में है। उसका काम भी दोहरा, तिहरा और चौहरा हो गया है।
उससे भी बड़ी बात यह है कि आज का रणस्थल बँटा हुआ नहीं है। यह नहीं कि कौरवों का महल एक जगह हो, पाण्डवों का अन्तःपुरी दूसरी जगह और कुरुक्षेत्र इन दोनों से दूर किसी तीसरी जगह। जो भी उस कुरुक्षेत्र में नहीं है वह संजय अपने को युद्ध से बाहर मानकर तटस्थ विवरण देता जाए ऐसा भाग्य अब उसका नहीं रहा। अब कुरुक्षेत्र बहुत व्यापक है। हर जगह है। शस्त्रयुक्त योद्धाओं की रणभूमि में भी, पाण्डवों का अन्तःपुर में भी, कौरवों के प्रासाद में भी, यहाँ तक कि अर्जुन का रथ चलाते हुए कृष्ण के चिन्तन में भी है, और दूर छुटी हुई यमुना-तट की किसी ग्राम बालिका के मन में भी। दो पक्षों का संघर्ष, दो नैतिकताओं का संघर्ष, दो दृष्टिकोणों का संघर्ष बराबर चलता रहता है। संजय कि तटस्थता बहुत उलझी हुई, जटिल प्रक्रिया हो गई है क्योंकि कभी-कभी संजय जो कहना चाहता है उसमें और जिन शब्दों से कहना चाहता है उनमें संघर्ष उठ खड़ा होता है। फिर भी उसका अटूट विश्वास है कि उसका एक रचनाकार व्यक्तित्व है जो भोक्ता भी है और तटस्थ दृष्टा भी। छाया की तरह बराबर वह व्यक्तित्व उसके साथ रहता है, उस तमाम दौरान में जब वह पानी की धार की तरह हजार-हजार रंग की नालियों में बेतहाशा पगलाया हुआ सा बहता जाता है।
कभी-कभी युद्ध से थक जाता है, जीवन के कठोर निर्मम संघर्ष से थक जाता है, लौट जाता है उस ठण्डी, ख़ुशनुमा नवम्बर की उजली भोर के कोहरे में !
असल में पद्मा जिज्जी मुझसे कुछ महीने छोटी हैं लेकिन केवल अपने तेहे, बेरोक हँसी और बुज़ुर्गाना ममता के बल पर बड़ी बन बैठी हैं। उसके बाद आज तक क्या मजाल कि उन्होंने कभी एक पल को यह माना हो कि मैं उनसे बड़ा नहीं तो कम-से-कम उनके बराबर का तो हूँ ही या अब मैं उम्र के साथ-साथ थोड़ा समझदार हो चला हूँ। समझदारी की बात मैंने उठायी कि उन्होंने खिलखिलाकर हँसना शुरू कर दिया। हँसी के बीच-बीच में मेरी जाने कौन-कौन-सी मनोरंजक भूलों की मनगढ़न्त कहानियाँ नमक-मिर्च लगाकर सुनाएँगी और फिर खिलखिलाकर हँसेंगी। नतीजा यह होगा कि डर के मारे उनका बड़प्पन मुझे फिर स्वीकार कर लेना पड़ेगा और उनके आदेशों का आँख मूँदकर पालन करना पड़ेगा।
उन दिनों उनको झक सवार थी मेरी तन्दुरस्ती सुधरवाने की। सेठ (मेरे बहनोई साहब) का तबादला जिला बाराबंकी के एक बड़े ख़ूबसूरत गाँव में हो गया था, जिसके चारों ओर पहाड़ियाँ और घने जंगल थे। एक छोटी-सी रेलवे लाइन उधर से गुजरती थी। कई मील दूर बियावान जंगल में चौड़ी गहरी खतरनाक मटमैली सरजू नदी बहती थी, जिस पर रेल का बहुत बड़ा पुराना पुल था। पटरियों के किनारे-किनारे जाइए तो चारों ओर लोहे के जाल से बना हुआ धुएँ से काला पड़ा वह पुल एक भयानक कन्दरा-जैसा लगता था। वह कन्दरा उस खौफनाक विराट् जंगली नदी को चीर कर न जाने कहाँ ट्रेनों को ले जाती थी। पद्मा जिज्जी ख़ुद कभी अपने घर से बाहर निकलकर दो फर्लांग भी नहीं गयी होंगी क्योंकि बड़ी अफसराइन थीं। कस्बे पर पुराने जमाने की स्पष्ट छाप थी और कोई महिला घर से नहीं निकलती थी।
लेकिन मेरी तन्दुरस्ती सुधरनी तो जरूरी थी। इसलिए सुबह मेरा चार मील टहलना भी जरूरी था। उस दिन तड़के अँधरे मुँह जिज्जी की डाँट सुनाई पड़ी और बची-खुची तन्दुरस्ती को बढ़ाने के लिए मैं पटरियों के किनारे-किनारे प्रातः भ्रमण के नाम पर जिज्ञासु सिद्धार्थ की तरह घर से निकल पड़ा।
अवध की सुबह, हवाएँ सीधे हिमलय से आती हैं। माथे पर टकराती है, पलकों को, होठों से छूती है, बालों को बिखेरती हैं और चारों ओर छाये हुए कोहरे में हल्की-हल्की लहरें बनती चली जाती हैं। ज्यों-ज्यों सुबह होती है, कुहरा घना लगने लगता है। फिर उसमें परतें बन जाती हैं; फिर कहीं पेड़ों के बीच, कहीं लाइन के पास, कहीं सरोवर में ऊपर कोहरे के बड़े-बड़े टुकड़े जमा हो जाते हैं। लाइन के किनारे-किनारे छोटे-छोटे पोखरे लगातार चले गये थे जिसमें कई रंग के छोटे-छोटे कुमुद, कोकाबेली और कमल फैले थे। लाइन के उस ओर सूरज उग रहा था। लाइन ऊँचाई पर थी और मेरी छाया बहुत लम्बी, धुँधली भूरी धारी की तरह कोहरे में तैरती जा रही थी। दिन और ज्यादा खिला, छाया जरा छोटी हुई, नीचे उतरी और किनारे सरोवरों के कोहरे में ढँके कमल और कोकाबेली के फूलों पर से तैरती हुई चलने लगी। मैं कुछ सोच नहीं रहा था सिर्फ यह महसूस कर रहा था कि सरोवर का ठण्डा पानी, कमल का हरियाला ताजा स्पर्श, सिवार का उलझाव—अब मुझमें से गुजर रहा है। दोनों में मैं हूँ, कंकड़ और लोहे के इस रास्ते पर चलता हुआ मैं और कोहरे, कमल और सरोवर में तैरता हुआ मैं। और मैं सिहर कर रुक गया, जब मैंने देखा कि किनारे से दो-जल साँप छप्प से कूदे और मेरी पूरी छाँह को पानी में सौ-सौ टुकड़ो में काटते हुए, टेढ़े-मेढ़े लहराते-तैरते हुए कमल-नाल के चारों ओर खेलने लगे, जहाँ मेरा छाया कण्ठ था। मैंने दोनों हाथ अपने ठण्डे, सुबह की ओस से भीगे गले पर रखे। साँप कमल-नाल को लपेटकर आपस में कुलेल कर रहे थे।
मैं नहीं जानता, सौन्दर्य किसे कहते हैं। यह जानता हूँ कि कुछ चीजें बाँध लेती हैं। उस दिन सुबह उन साँपों ने मुझे बाँध लिया था। जादू तब टूटा जब लखनऊ से आने वाली गाड़ी की सीटी दूर से सुनाई दी। लौटकर आया तो जिज्जी परेशान थीं। दो अर्दली साइकिल पर मेरी खोज में जा चुके थे।
घर के बगल में टीलों को काटता हुआ एक नाला बहता था। किनारे-किनारे एक पगडण्डी थी जो जंगल के बीचोंबीच ले जाती थी। जंगल का वह छोटा-सा हिस्सा खेतों के समुद्र में हरे प्रायद्वीप की तरह घुस आया था। लेकिन कितना भयानक था वह जंगल ! लतरों ने नीचे से उगकर, तनों से लिपटकर, ऊपर डालियों से झूल-झूलकर जंगल को भयानकतम बना दिया था। घर-भर को खिला-पिला कर जिज्जी सो जाती थीं तो मैं वहाँ भाग जाता था। उस दिन दो डालों के बीच बैठा-बैठा कुछ सोचता रहा। वह ‘मैं’ कौन है जो अपने से अलग जीता है ? कमल और साँपों से खेलता है और उसका एक-एक संवेदन मुझ तक पहुँचा देता है ? या यह केवल छाया है ? उन दोनों का एकत्व कहाँ होता है ? किशोर के मन में पहली बार अपने अन्दर की भाव-प्रतिक्रिया के प्रति कुतूहल जागा था। याद है मुझे कि दो तीन दिन अजीब बेचैनी और अजब भावाकुलता मन में बनी रही। बहुत दिनों बाद एक कविता लिखी थी—झील के किनारे :
उससे भी बड़ी बात यह है कि आज का रणस्थल बँटा हुआ नहीं है। यह नहीं कि कौरवों का महल एक जगह हो, पाण्डवों का अन्तःपुरी दूसरी जगह और कुरुक्षेत्र इन दोनों से दूर किसी तीसरी जगह। जो भी उस कुरुक्षेत्र में नहीं है वह संजय अपने को युद्ध से बाहर मानकर तटस्थ विवरण देता जाए ऐसा भाग्य अब उसका नहीं रहा। अब कुरुक्षेत्र बहुत व्यापक है। हर जगह है। शस्त्रयुक्त योद्धाओं की रणभूमि में भी, पाण्डवों का अन्तःपुर में भी, कौरवों के प्रासाद में भी, यहाँ तक कि अर्जुन का रथ चलाते हुए कृष्ण के चिन्तन में भी है, और दूर छुटी हुई यमुना-तट की किसी ग्राम बालिका के मन में भी। दो पक्षों का संघर्ष, दो नैतिकताओं का संघर्ष, दो दृष्टिकोणों का संघर्ष बराबर चलता रहता है। संजय कि तटस्थता बहुत उलझी हुई, जटिल प्रक्रिया हो गई है क्योंकि कभी-कभी संजय जो कहना चाहता है उसमें और जिन शब्दों से कहना चाहता है उनमें संघर्ष उठ खड़ा होता है। फिर भी उसका अटूट विश्वास है कि उसका एक रचनाकार व्यक्तित्व है जो भोक्ता भी है और तटस्थ दृष्टा भी। छाया की तरह बराबर वह व्यक्तित्व उसके साथ रहता है, उस तमाम दौरान में जब वह पानी की धार की तरह हजार-हजार रंग की नालियों में बेतहाशा पगलाया हुआ सा बहता जाता है।
कभी-कभी युद्ध से थक जाता है, जीवन के कठोर निर्मम संघर्ष से थक जाता है, लौट जाता है उस ठण्डी, ख़ुशनुमा नवम्बर की उजली भोर के कोहरे में !
असल में पद्मा जिज्जी मुझसे कुछ महीने छोटी हैं लेकिन केवल अपने तेहे, बेरोक हँसी और बुज़ुर्गाना ममता के बल पर बड़ी बन बैठी हैं। उसके बाद आज तक क्या मजाल कि उन्होंने कभी एक पल को यह माना हो कि मैं उनसे बड़ा नहीं तो कम-से-कम उनके बराबर का तो हूँ ही या अब मैं उम्र के साथ-साथ थोड़ा समझदार हो चला हूँ। समझदारी की बात मैंने उठायी कि उन्होंने खिलखिलाकर हँसना शुरू कर दिया। हँसी के बीच-बीच में मेरी जाने कौन-कौन-सी मनोरंजक भूलों की मनगढ़न्त कहानियाँ नमक-मिर्च लगाकर सुनाएँगी और फिर खिलखिलाकर हँसेंगी। नतीजा यह होगा कि डर के मारे उनका बड़प्पन मुझे फिर स्वीकार कर लेना पड़ेगा और उनके आदेशों का आँख मूँदकर पालन करना पड़ेगा।
उन दिनों उनको झक सवार थी मेरी तन्दुरस्ती सुधरवाने की। सेठ (मेरे बहनोई साहब) का तबादला जिला बाराबंकी के एक बड़े ख़ूबसूरत गाँव में हो गया था, जिसके चारों ओर पहाड़ियाँ और घने जंगल थे। एक छोटी-सी रेलवे लाइन उधर से गुजरती थी। कई मील दूर बियावान जंगल में चौड़ी गहरी खतरनाक मटमैली सरजू नदी बहती थी, जिस पर रेल का बहुत बड़ा पुराना पुल था। पटरियों के किनारे-किनारे जाइए तो चारों ओर लोहे के जाल से बना हुआ धुएँ से काला पड़ा वह पुल एक भयानक कन्दरा-जैसा लगता था। वह कन्दरा उस खौफनाक विराट् जंगली नदी को चीर कर न जाने कहाँ ट्रेनों को ले जाती थी। पद्मा जिज्जी ख़ुद कभी अपने घर से बाहर निकलकर दो फर्लांग भी नहीं गयी होंगी क्योंकि बड़ी अफसराइन थीं। कस्बे पर पुराने जमाने की स्पष्ट छाप थी और कोई महिला घर से नहीं निकलती थी।
लेकिन मेरी तन्दुरस्ती सुधरनी तो जरूरी थी। इसलिए सुबह मेरा चार मील टहलना भी जरूरी था। उस दिन तड़के अँधरे मुँह जिज्जी की डाँट सुनाई पड़ी और बची-खुची तन्दुरस्ती को बढ़ाने के लिए मैं पटरियों के किनारे-किनारे प्रातः भ्रमण के नाम पर जिज्ञासु सिद्धार्थ की तरह घर से निकल पड़ा।
अवध की सुबह, हवाएँ सीधे हिमलय से आती हैं। माथे पर टकराती है, पलकों को, होठों से छूती है, बालों को बिखेरती हैं और चारों ओर छाये हुए कोहरे में हल्की-हल्की लहरें बनती चली जाती हैं। ज्यों-ज्यों सुबह होती है, कुहरा घना लगने लगता है। फिर उसमें परतें बन जाती हैं; फिर कहीं पेड़ों के बीच, कहीं लाइन के पास, कहीं सरोवर में ऊपर कोहरे के बड़े-बड़े टुकड़े जमा हो जाते हैं। लाइन के किनारे-किनारे छोटे-छोटे पोखरे लगातार चले गये थे जिसमें कई रंग के छोटे-छोटे कुमुद, कोकाबेली और कमल फैले थे। लाइन के उस ओर सूरज उग रहा था। लाइन ऊँचाई पर थी और मेरी छाया बहुत लम्बी, धुँधली भूरी धारी की तरह कोहरे में तैरती जा रही थी। दिन और ज्यादा खिला, छाया जरा छोटी हुई, नीचे उतरी और किनारे सरोवरों के कोहरे में ढँके कमल और कोकाबेली के फूलों पर से तैरती हुई चलने लगी। मैं कुछ सोच नहीं रहा था सिर्फ यह महसूस कर रहा था कि सरोवर का ठण्डा पानी, कमल का हरियाला ताजा स्पर्श, सिवार का उलझाव—अब मुझमें से गुजर रहा है। दोनों में मैं हूँ, कंकड़ और लोहे के इस रास्ते पर चलता हुआ मैं और कोहरे, कमल और सरोवर में तैरता हुआ मैं। और मैं सिहर कर रुक गया, जब मैंने देखा कि किनारे से दो-जल साँप छप्प से कूदे और मेरी पूरी छाँह को पानी में सौ-सौ टुकड़ो में काटते हुए, टेढ़े-मेढ़े लहराते-तैरते हुए कमल-नाल के चारों ओर खेलने लगे, जहाँ मेरा छाया कण्ठ था। मैंने दोनों हाथ अपने ठण्डे, सुबह की ओस से भीगे गले पर रखे। साँप कमल-नाल को लपेटकर आपस में कुलेल कर रहे थे।
मैं नहीं जानता, सौन्दर्य किसे कहते हैं। यह जानता हूँ कि कुछ चीजें बाँध लेती हैं। उस दिन सुबह उन साँपों ने मुझे बाँध लिया था। जादू तब टूटा जब लखनऊ से आने वाली गाड़ी की सीटी दूर से सुनाई दी। लौटकर आया तो जिज्जी परेशान थीं। दो अर्दली साइकिल पर मेरी खोज में जा चुके थे।
घर के बगल में टीलों को काटता हुआ एक नाला बहता था। किनारे-किनारे एक पगडण्डी थी जो जंगल के बीचोंबीच ले जाती थी। जंगल का वह छोटा-सा हिस्सा खेतों के समुद्र में हरे प्रायद्वीप की तरह घुस आया था। लेकिन कितना भयानक था वह जंगल ! लतरों ने नीचे से उगकर, तनों से लिपटकर, ऊपर डालियों से झूल-झूलकर जंगल को भयानकतम बना दिया था। घर-भर को खिला-पिला कर जिज्जी सो जाती थीं तो मैं वहाँ भाग जाता था। उस दिन दो डालों के बीच बैठा-बैठा कुछ सोचता रहा। वह ‘मैं’ कौन है जो अपने से अलग जीता है ? कमल और साँपों से खेलता है और उसका एक-एक संवेदन मुझ तक पहुँचा देता है ? या यह केवल छाया है ? उन दोनों का एकत्व कहाँ होता है ? किशोर के मन में पहली बार अपने अन्दर की भाव-प्रतिक्रिया के प्रति कुतूहल जागा था। याद है मुझे कि दो तीन दिन अजीब बेचैनी और अजब भावाकुलता मन में बनी रही। बहुत दिनों बाद एक कविता लिखी थी—झील के किनारे :
वह निरन्तर जो कि चलता आ रहा है साथ
इन सबों से सर्वथा निरपेक्ष
लापरवाह
नीली झील के इस छोर से
उस छोर तक
एक जादू के सपन-सा
तैरता जाता
इन सबों से सर्वथा निरपेक्ष
लापरवाह
नीली झील के इस छोर से
उस छोर तक
एक जादू के सपन-सा
तैरता जाता
उस दिन यह बोध कुतूहल, विस्मय और व्यक्तित्व की आन्तरिक सम्पन्नता के
प्रति एक महत्त्वपूर्ण खुशी जागी थी। लेकिन ज्यों-ज्यों वक्त बीतता गया
मालूम हुआ कि संजय का काम इतना आसान नहीं है। वे लड़ते हुए छाया शरीर को
सौ-सौ खण्डों में काटते हुए जल-साँप इतने निरापद विषहीन भी नहीं है। यह भी
मालूम हुआ कि बहुत सुबह जंगली नदी की ओर निकल जानेवाले के लिए फिर कोई ऐसा
ममता भरा घर नहीं बचता जहाँ लौटकर वह ममता की छाँह में सब भूल जाए। ऐसा
कोई शान्त अरण्य नहीं है जहाँ वह बैठकर चुपचाप सोच सके। सबकुछ खण्ड-खण्ड
होकर घुल-मिल गया है। छायाएँ साँप बन जाती हैं, कमल की पँखुरियाँ खँख्वार
नदी बन जाती हैं नदियाँ उन घरों को सैलाब में बहा ले जाती हैं जहाँ थके
पाँव लौटा करते हैं और जिन शक्ति अरण्यों में लौटकर चुपचाप चिन्तन किया जा
सकता है वे अरण्य छाया की तरह समानान्तर चलते हैं, उनको देखते रहिए पर
उसमें लौटकर चिन्तन नहीं कर सकते। और फिर साँपों की लताएँ, जंगली नदियों
का तूफान, कुहरा सब एक विराट जंगल बन जाते हैं जिनमें लौटने का कोई रास्ता
नहीं।
लेकिन संजय की समस्या है कि उसे पीछे लौटना भी है ! दिक् की सीमाओं की तरह काल की सीमाओं को भी तोड़ना है, समय प्रवाह में आगे भी बढ़ना है, पीछे भी लौटना है और कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे लौटना है और कभी-कभी पीछे लौटने की ही प्रक्रिया में ही आगे बढ़ते जाना है।
विचित्र है यह आधुनिक युग का माहौल जिसमें जिज्ञासा एक पहलू से देखने पर ऋषियों की दिव्य दृष्टि लगे और दूसरे पहलू से सरकस के खिलाड़ियों का हास्यपद व्यायाम ! आस्था से श्रद्धापूर्वक सिर झुकाइए और होठों पर बरबस हँसी आती जाए ! और तुर्रा यह कि तटस्थ संजय तटस्थ भी नहीं है और पक्षधर भी नहीं। कृष्ण की तरह इस सारे युद्ध में सिर्फ वही मरता है, हर बार वही मरता है। चाहे किसी का ब्रह्मास्त्र छूटे, चाहे किसी की गदा चले, चाहे किसी धृतराष्ट का प्रवंचना-भरा लौह आलिंगन मिले, मृत्यु उसी की होती है। वह शिकायत भी नहीं कर सकता क्योंकि उसको मारने वाले के मन में भी जो-जो भटकन और बेचैनी है, किसी अंश में संजय का उसके साथ भी तादात्म्य है।
(3)
लेकिन संजय की समस्या है कि उसे पीछे लौटना भी है ! दिक् की सीमाओं की तरह काल की सीमाओं को भी तोड़ना है, समय प्रवाह में आगे भी बढ़ना है, पीछे भी लौटना है और कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे लौटना है और कभी-कभी पीछे लौटने की ही प्रक्रिया में ही आगे बढ़ते जाना है।
विचित्र है यह आधुनिक युग का माहौल जिसमें जिज्ञासा एक पहलू से देखने पर ऋषियों की दिव्य दृष्टि लगे और दूसरे पहलू से सरकस के खिलाड़ियों का हास्यपद व्यायाम ! आस्था से श्रद्धापूर्वक सिर झुकाइए और होठों पर बरबस हँसी आती जाए ! और तुर्रा यह कि तटस्थ संजय तटस्थ भी नहीं है और पक्षधर भी नहीं। कृष्ण की तरह इस सारे युद्ध में सिर्फ वही मरता है, हर बार वही मरता है। चाहे किसी का ब्रह्मास्त्र छूटे, चाहे किसी की गदा चले, चाहे किसी धृतराष्ट का प्रवंचना-भरा लौह आलिंगन मिले, मृत्यु उसी की होती है। वह शिकायत भी नहीं कर सकता क्योंकि उसको मारने वाले के मन में भी जो-जो भटकन और बेचैनी है, किसी अंश में संजय का उसके साथ भी तादात्म्य है।
(3)
क्रान्तिद्रष्टा नहीं हैं हम
मनीषी भी नहीं
मसीहा भी नहीं
पर, ओ भाई...
मनीषी भी नहीं
मसीहा भी नहीं
पर, ओ भाई...
मलयज
अच्छे थे वह जमाने जब दुनिया में मसीहा हुआ करते थे। एक ओर काफी गुनाह
होते रहते थे, धर्म, नियम टूटते रहते थे, और दूसरी ओर कोई मसीहा आता था जो
ख़ुद ईश्वर होता था, हाथ उठाकर कहता था कि सारे संशय छोड़कर मेरी शरण में
आओ। तुम्हारा समस्त ‘योग-क्षेम वहाम्यहम्’ या कोई
दूसरा मसीहा
आता था जो ईश्वर नहीं ईश्वर का बेटा होता था और कहता था, तमाम दुनिया के
पाप मैंने अपने कन्धे पर ले लिए हैं ताकि हे पिता, ये तुम्हारे तईं
विश्वास लाएँ और तू इन्हें क्षमा करे। कवि भी छोटा-मोटा मसीहा होता था :
‘कविर्मनीषी परिभूस्वयंभू’— पोयेट दॅ
अनअक्नॉलेज्ड
लेज़िस्लेटर ऑफ़ दॅ वर्ल्ड।’
जमाना बदल गया है जमाने का मिजाज बदल गया है। मसीहे निर्थक लगने लगे हैं और ‘योग-क्षेम वहाम्यहम्’-जैसे मसीहाई वाक्य भारतीय जीवन-बीमा
निगम के मोटे वाक्य बन चुके हैं। और हस्तिनापुर में ‘कविर्मनीषी’ का क्या हुआ उसका न जानना ही अच्छा है।
संजय मसीहाई के गर्व से यह नहीं कह सकता कि सबका पाप अपने कन्धों पर लेकर उसने कोई बहुत बड़ा काम किया है, न वह पूर्ण प्रभु और अपूर्ण जनसाधारण के बीच का जनसम्पर्क अधिकारी है। मसीहा ऊपर से आता था और बड़ी-बड़ी सभ्यताओं का कूड़ा कचरा बटोरकर फिर ऊपर चला जाता था; तब तक के लिए जब तक कि वह कूड़-कचरा फिर न इकट्ठा हो जाए। संजय ने यह जाना कि नये युग के मिजाज का एक नया रंग निराला है जो गुलाब के मुकाबले में कूड़े-कचरे या उस पर उगे कुकुरमुत्ते को तरजीह देने लगा है। दूसरी आवाज पन्त की है, ‘‘कूड़ा-कर्कट’ सब भू पर : लगता सार्थ और सुन्दर !’’ और लो स्याह–से, पवित्र-मलिन, अच्छे बुरे की तमाम धारणाएँ सदियों से जमी-जमायी बिखर गयी हैं। मसीहाई के जमाने में तो बिल्कुल स्पष्ट मालूम होता था कि एक पक्ष मर्यादा का होता है और दूसरा पक्ष अमर्यादा का, एक पक्ष का विनाश जरूरी है और दूसरे पक्ष का उद्धार। मगर यह कैसा अजब वातावरण है कि अच्छे और बुरे के बीच की रेखा बिल्कुल अनिश्चित है। मर्यादा अगर टूटती है तो उसको तोड़ने में भी सहयोगी है—कोई कुछ कम, कोई कुछ ज्यादा ! ‘टुकड़े-टुकड़े हो बिखर गई मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है, पाण्डव ने कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज्यादा !’’ और तब कोई भी ऐसा मसीहा नहीं रह जाता जो सामन्य संकट से निर्लिप्त सर्वोपरि हो और उस उलझन में दीख पड़ता है कि कृष्ण की मौत तथा परीक्षित की मौत एक ही कहानी के दो अध्याय बन जाते हैं।
और यहाँ से उसकी खोज फिर से शुरू हो जाती है। यह खोज इतनी जटिल और इतनी कठिन है जितनी कि शायद पहले कभी नहीं रही। तमाम चीजों को देखने, उनकी अच्छा-बुराई परखने का जो अन्दरूनी मापदण्ड था यह झूठा पड़ चुका है। हर युद्ध उसके बाहर भी होता है और उसके मन में भी। वह मरने वाला भी है और जिस उपकरण ने मारा है वह भी उसी का है। वह परीक्षित भी है और अश्वत्थामा भी। इन सबके बीच से उसे चीजों का अर्थ खोजना है। बाहरी निगाह वालों के लिए दुनिया पहले से कहीं ज्यादा ख़ुशनुमा, रंगीन और जगमग है। लेकिन उसके लिए वह रोशनी बुझ चुकी है जिससे दुनिया की तमाम रोशनियाँ देखी जाती हैं : तमाम रंग पहचाने जाते हैं।
मेरे शहर में एक नुमायश आती थी। उस छोटे उजाड़ बियावान शहर में वह वर्ष का सबसे उल्लासमय पर्व होता था। साल दर साल वही पुरानी दुकानें, वही बिजलियों का सजाव, वही शिवमूर्ति की जटाओं से निकलता फव्वारा ! मगर शहर का शहर उमड़ पड़ता था। उनके लिए वह सब हर बार नया था। उस दिन जालौन की मशहूर आतिशबाजी के खेल दिखाये जाने वाले थे। मेरे मोहल्ले का अन्धा बरेठा ग्राहकों के उधार के कपड़े पहनकर नुमायश में जाने के लिए तैयार हो रहा था। नुमायश की ठसाठस भीड़ में मैने उसे देखा। उसका लड़का उसका एक हाथ पकड़े था, धक्के खाता हुआ बाएँ हाथ से टटोलता-टटोलता वह अन्धा बरेठा नुमायश ‘देख’ (?) रहा था। थोड़ी देर में आतिशबाजियाँ छूटेंगी, आसमान में रोशनी के अजीबोगरीब खेल होंगे ! सौ-सौ रंगों के अनार छूटेंगे और मेरे मुहल्ले का अन्धा बरेठा उन्हें ‘देखेगा’ ! हाय रे उजाले की प्यास !
जमाना बदल गया है जमाने का मिजाज बदल गया है। मसीहे निर्थक लगने लगे हैं और ‘योग-क्षेम वहाम्यहम्’-जैसे मसीहाई वाक्य भारतीय जीवन-बीमा
निगम के मोटे वाक्य बन चुके हैं। और हस्तिनापुर में ‘कविर्मनीषी’ का क्या हुआ उसका न जानना ही अच्छा है।
संजय मसीहाई के गर्व से यह नहीं कह सकता कि सबका पाप अपने कन्धों पर लेकर उसने कोई बहुत बड़ा काम किया है, न वह पूर्ण प्रभु और अपूर्ण जनसाधारण के बीच का जनसम्पर्क अधिकारी है। मसीहा ऊपर से आता था और बड़ी-बड़ी सभ्यताओं का कूड़ा कचरा बटोरकर फिर ऊपर चला जाता था; तब तक के लिए जब तक कि वह कूड़-कचरा फिर न इकट्ठा हो जाए। संजय ने यह जाना कि नये युग के मिजाज का एक नया रंग निराला है जो गुलाब के मुकाबले में कूड़े-कचरे या उस पर उगे कुकुरमुत्ते को तरजीह देने लगा है। दूसरी आवाज पन्त की है, ‘‘कूड़ा-कर्कट’ सब भू पर : लगता सार्थ और सुन्दर !’’ और लो स्याह–से, पवित्र-मलिन, अच्छे बुरे की तमाम धारणाएँ सदियों से जमी-जमायी बिखर गयी हैं। मसीहाई के जमाने में तो बिल्कुल स्पष्ट मालूम होता था कि एक पक्ष मर्यादा का होता है और दूसरा पक्ष अमर्यादा का, एक पक्ष का विनाश जरूरी है और दूसरे पक्ष का उद्धार। मगर यह कैसा अजब वातावरण है कि अच्छे और बुरे के बीच की रेखा बिल्कुल अनिश्चित है। मर्यादा अगर टूटती है तो उसको तोड़ने में भी सहयोगी है—कोई कुछ कम, कोई कुछ ज्यादा ! ‘टुकड़े-टुकड़े हो बिखर गई मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है, पाण्डव ने कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज्यादा !’’ और तब कोई भी ऐसा मसीहा नहीं रह जाता जो सामन्य संकट से निर्लिप्त सर्वोपरि हो और उस उलझन में दीख पड़ता है कि कृष्ण की मौत तथा परीक्षित की मौत एक ही कहानी के दो अध्याय बन जाते हैं।
और यहाँ से उसकी खोज फिर से शुरू हो जाती है। यह खोज इतनी जटिल और इतनी कठिन है जितनी कि शायद पहले कभी नहीं रही। तमाम चीजों को देखने, उनकी अच्छा-बुराई परखने का जो अन्दरूनी मापदण्ड था यह झूठा पड़ चुका है। हर युद्ध उसके बाहर भी होता है और उसके मन में भी। वह मरने वाला भी है और जिस उपकरण ने मारा है वह भी उसी का है। वह परीक्षित भी है और अश्वत्थामा भी। इन सबके बीच से उसे चीजों का अर्थ खोजना है। बाहरी निगाह वालों के लिए दुनिया पहले से कहीं ज्यादा ख़ुशनुमा, रंगीन और जगमग है। लेकिन उसके लिए वह रोशनी बुझ चुकी है जिससे दुनिया की तमाम रोशनियाँ देखी जाती हैं : तमाम रंग पहचाने जाते हैं।
मेरे शहर में एक नुमायश आती थी। उस छोटे उजाड़ बियावान शहर में वह वर्ष का सबसे उल्लासमय पर्व होता था। साल दर साल वही पुरानी दुकानें, वही बिजलियों का सजाव, वही शिवमूर्ति की जटाओं से निकलता फव्वारा ! मगर शहर का शहर उमड़ पड़ता था। उनके लिए वह सब हर बार नया था। उस दिन जालौन की मशहूर आतिशबाजी के खेल दिखाये जाने वाले थे। मेरे मोहल्ले का अन्धा बरेठा ग्राहकों के उधार के कपड़े पहनकर नुमायश में जाने के लिए तैयार हो रहा था। नुमायश की ठसाठस भीड़ में मैने उसे देखा। उसका लड़का उसका एक हाथ पकड़े था, धक्के खाता हुआ बाएँ हाथ से टटोलता-टटोलता वह अन्धा बरेठा नुमायश ‘देख’ (?) रहा था। थोड़ी देर में आतिशबाजियाँ छूटेंगी, आसमान में रोशनी के अजीबोगरीब खेल होंगे ! सौ-सौ रंगों के अनार छूटेंगे और मेरे मुहल्ले का अन्धा बरेठा उन्हें ‘देखेगा’ ! हाय रे उजाले की प्यास !
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book