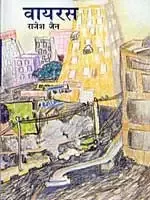|
नाटक-एकाँकी >> वायरस वायरसराजेश जैन
|
407 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है वायरस...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
गत बीस वर्षों से हिन्दी साहित्य-सृजन से अनवरत जुड़े राजेश जैन के
‘हिन्दी मास्टर’, ‘चिमनी चोगा’ एवं अन्य दर्जनों
नाटकों की श्रृंखला में ‘वायरस’ उनकी नवीनतम् नाट्य-कृति है।
महानगरीय त्रासदी एवं दाम्पत्य मूल्यों का विद्रूपात्मक ह्रास यूँ तो यह विडम्बना आधुनिक उपभोक्ता संस्कृति से अनुप्राणित तकनीकी बिम्ब की प्रयोगधर्मिता का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आयी है। लेखक की अन्य रचनाओं की भाँति इसमें भी आधुनिक समाज की बाह्य और आन्तरिक दुर्बलताओं पर तीखा व्यंग्य है।
मंचीय नाटक के क्षेत्र में हिन्दी कृतियों के अभाव की दुहाई देने वाले रंगकर्मियों के लिए यह रंचना एक सार्थक चुनौती दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
महानगरीय त्रासदी एवं दाम्पत्य मूल्यों का विद्रूपात्मक ह्रास यूँ तो यह विडम्बना आधुनिक उपभोक्ता संस्कृति से अनुप्राणित तकनीकी बिम्ब की प्रयोगधर्मिता का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आयी है। लेखक की अन्य रचनाओं की भाँति इसमें भी आधुनिक समाज की बाह्य और आन्तरिक दुर्बलताओं पर तीखा व्यंग्य है।
मंचीय नाटक के क्षेत्र में हिन्दी कृतियों के अभाव की दुहाई देने वाले रंगकर्मियों के लिए यह रंचना एक सार्थक चुनौती दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
नाट्यभूमि
वायरस : विसंगत मूल्यों का कम्प्यूटरीकरण
वायरस : विसंगत मूल्यों का कम्प्यूटरीकरण
चाहता था, नाटक ‘वायरस’ के प्रकाशन के साथ भूमिकानुमा
चीज़
आदरणीय नेमिचन्द्र जैन के सौजन्य से जाये। गत कई वर्षों से स्नेहपूर्ण
अंतरंगता के कारण अपनी माँग मैंने सहजता से उनके समक्ष रख दी-क्योंकि
‘वायरस’ की नाट्य प्रक्रिया में उनका परिपक्व
हस्तक्षेप,
श्रीराम सेण्टर की कार्यशाला के कारण रहा है। कार्यशाला का संचालन नेमि जी
ने किया था। जब नाटक का प्रारूप भेजने का आमन्त्रण मिला तो अर्से से
उद्वेलित हो रहे सोच को एक दिशा-सी मिल गयी। कथानक का आइडिया बहुत पहले
सूझ गया था, जब-तब उसमें जोड़तोड़ चलती रहती थी। परिवेश की उर्वरता से
तकनीकी तौर पर साहित्यिक बिम्बों का दोहन करने की मेरी प्रवृत्ति सहज और
स्वभावत: है........और दरअसल इस कथानक पर उपन्यास लिखने का मेरा ज्यादा
इरादा था, किन्तु एकाएक नाटक की कार्यशाला का प्रस्ताव आया तो थीम का
नाट्य-विधा द्वारा अपहरण हो गया। नाटक का धुँधला ख्याल ज़रूर था पर उसमें
गंभीरता नेमि जी के आमन्त्रण से ही आयी। उपन्यास का नाट्यान्तर परम्परागत
तौर पर होता ही रहा है......पर मैंने सोचा-क्यों न पहले नाटक बना
लूँ.........फिर वक्त और प्रेरणा मिलने पर नाटक का उपन्यासीकरण भी कर लिया
जायेगा। कार्यशाला में नाटक-पाठ के बाद कई उपयोगी सुझाव मिले। बाद में एक
बारगी उन सुझावों के अनुकूल संशोधन भी कर डाले। फिर मुझे ज्यादा उचित यह
लगा कि प्रकाशन के लिए नाटक की मूल पाण्डुलिपि यथावत् ही रहे- हाँ, मंचन
के समय निदेशक से विचार-विमर्श करके परिवर्तन किये जा रहे हैं-अन्यथा
परिवर्तनों (बनाम इनोवेशन) का कोई अन्त नहीं है-यह एक अनवरत प्रक्रिया है,
जिसके फ्रीज न होने में उसकी सार्थकता है।
आमुख-कथन के अनुरोध को नेमी जी ने विनम्रता से टाल दिया। उनसे मुझे भूमिका नहीं मिली पर एक नयी चीज़ अवश्य मिली। उन्होंने कहा-‘‘मैं किसी भी पुस्तक की भूमिका लिखने या लिखवाने का पक्षधर नहीं हूँ-नियम-सा है कि मैं किसी की भूमिका नहीं लिखता। दरअसल युवा लेखकों को मेरी यह सलाह होती है कि अपनी पुस्तक की भूमिका आदि किसी से न लिखवायें, वरन् कृति को अपने बलबूते पर ही खड़ा होने दें-स्वतन्त्र रूप से।’’
‘‘तो क्या लेखक को स्वयं भी भूमिकानुमा आलेख नहीं लिखना चाहिए ?’’- मेरा सवाल था।
‘‘लेखक चाहे तो अवश्य लिखे क्योंकि उससे रचना-प्रक्रिया का आभास मिलता है और रचना ज्यादा मज़बूत होती है......’’- नेमि जी का उत्तर था।
सो, अब स्वयं अपनी बात कह रहा हूँ। नाटक मैं बीस वर्षों से लिख रही हूँ। उन प्रारम्भिक दिनों में नाट्य-क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का जलजला मचा था-मोहन राकेश के ‘आधे-अधूरे’ की अलग पहचान बन रही थी। विघटित परिवार एवं दाम्पत्य जटिलताओं का सशक्त स्वर था उस नाटक में। समय के साथ सामाजिक एवं पारिवारिक परिवेश में बहुत परिवर्तन आ गये, संस्कृति में टेक्नोलॉजी का दखल भी बढ़ता ही जा रहा है, सामाजिक विद्रूपताओं एवं दाम्पत्य जीवन की असमान जटिलताओं को लेकर कोई रचना गढ़ने का संकल्प मेरी चेतना के गर्भ में पल रहा था, तभी एकाएक कम्प्यूटरीकरण सर्वत्र छाने लगा। कम्प्यूटर की शब्दावली में ‘वायरस’ वह प्रक्रिया है जो अगर लग जाये तो उपकरण के सामान्य व्यवहार में उलटफेर कर देती है, अजीब से विकृत और बेतरतीब परिणाम उभरने लगते हैं !
मेरी साहित्यिक संवेदना ऐसे प्रसंगों से मूलत: आबद्ध रही है-‘स्पेयर पार्टस’ ‘बूस्टर चालू आहे’, ‘रिमोट कंट्रोल’, ‘उत्प्रेरक’ ‘क्रैश’ आदि कहानियाँ इसी से प्रवृत्त हैं। साहित्य में जब राजनीति घुसपैठ कर सकती है तो तकनीकी विम्ब क्यों पीछे रहें ? बस लगा कि ऐसी मानवीय विसंगति का ‘वायरस’ किसी घर को भी लग सकता है.......दाम्पत्य जीवन, दिमाग़, विचार, किसी पर कोई क्षण ग्रन्थि या स्थिति वायरस के रूप में आक्रमण कर देते है और परिणाम में जो जद्दोजहद प्रसूत होती है, उसका एक अदना उदाहरण है संलग्न नाटक-‘वायरस’। ‘धक्का पम्प’, ‘व्याकरण’, ‘अन्धकूप’, ‘चिन्दी मास्टर’ एवं ‘चिमनी चोगा’ के बाद लिखे गये नवीनतम नाटक ‘वायरस’ को अपनी प्रिय रचना मानता हूँ......जिन रंगकर्मियों ने इसे पढ़ा,
सभी को विषय-वस्तु एवं उसकी प्रयोगशीलता पसन्द आयी है। रचनाओं के लिए पात्रों को पैदा करना भूत-प्रेतों को जगाने जैसा है। जगाने के बाद उन्हें निभाना होता है, वर्ना विकृत प्रभाव पड़ सकते हैं। ऐसे अनेक भूतप्रेतों से खाली समय में मैं घिर जाता हूँ ! वन्दना और रंजना के चरित्रों का विरोधाभास, विवाह की ज्वलन्त सामाजिक समस्या आदि मुद्दों के कारण यह नि:संदेह एक आम घरेलू कथानक है......किन्तु तकनीकी बिम्ब एवं निदान के लिए सिर उठाते अनोखे उपक्रम का वास्तविक अन्तध्वर्स संपूर्ण स्थिति को नया प्रयोगात्मक आयाम दे पाये-ऐसा मेरा प्रयत्न रहा है।
पुस्तक के अन्त में लघुनाटक ‘धक्का पम्प’ भी यहाँ शामिल है ! सन्’ 75 के आसपास जब नाट्य आन्दोलन करवटें ले रहा था, तब लिखी गयी इस व्यंग्य नाटिका को अज्ञेय जी ने ‘नया-प्रतीक’ में छापा था। फिर इसके कई मंचन हुए। जनवरी ’77 में ये म.प्र. कलापरिषद् के तत्त्वाधान में आयोजित रंगशिविर के ‘छतरियाँ’ ‘अपरिभाषित’ तथा ‘एवं इन्द्रजित’ के साथ ‘धक्का-पम्प’ का निर्देशन श्री एम.के. रैना ने किया था और फिर प्रस्तुति कई शहरों में हुई। इसी तरह उन्हीं दिनों स्व. रमेश बक्षी के आवेश टैरेस थियेटर के तहत दिल्ली में हेमन्त मिश्र के निर्देशन में इसका मंचन हुआ।
‘मंच’ वास्तव में नाटक की सीमाओं का रेखांकन है। उन दिनों नाटक अपनी सीमाओं को तोड़कर दर्शकों के बीच घुल-मिलकर बैठने को लालायित हो रहे थे- ‘धक्का-पम्प’ इसी लालसा का उदाहरण है। इसके माध्यम से युवा वर्ग की अकर्मण्यता, आलस्य और उच्छृंखल प्रवृत्ति पर कुठाराघात के अलावा व्यक्ति और व्यवस्था की जड़ विसंगतियों पर चोट भी की गयी है ! इस पर अंग्रेजी में लिखी गयी एम.के. रैना की मूल टिप्पणी नाटिका के आरम्भ में जोड़ी जा रही है।
पुस्तक के रूप में इन कृतियों के उपलब्ध होने पर रंगकर्मियों की नाट्य संभावानाएँ बलवती होंगी-ऐसी मेरी कामना है।
आमुख-कथन के अनुरोध को नेमी जी ने विनम्रता से टाल दिया। उनसे मुझे भूमिका नहीं मिली पर एक नयी चीज़ अवश्य मिली। उन्होंने कहा-‘‘मैं किसी भी पुस्तक की भूमिका लिखने या लिखवाने का पक्षधर नहीं हूँ-नियम-सा है कि मैं किसी की भूमिका नहीं लिखता। दरअसल युवा लेखकों को मेरी यह सलाह होती है कि अपनी पुस्तक की भूमिका आदि किसी से न लिखवायें, वरन् कृति को अपने बलबूते पर ही खड़ा होने दें-स्वतन्त्र रूप से।’’
‘‘तो क्या लेखक को स्वयं भी भूमिकानुमा आलेख नहीं लिखना चाहिए ?’’- मेरा सवाल था।
‘‘लेखक चाहे तो अवश्य लिखे क्योंकि उससे रचना-प्रक्रिया का आभास मिलता है और रचना ज्यादा मज़बूत होती है......’’- नेमि जी का उत्तर था।
सो, अब स्वयं अपनी बात कह रहा हूँ। नाटक मैं बीस वर्षों से लिख रही हूँ। उन प्रारम्भिक दिनों में नाट्य-क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का जलजला मचा था-मोहन राकेश के ‘आधे-अधूरे’ की अलग पहचान बन रही थी। विघटित परिवार एवं दाम्पत्य जटिलताओं का सशक्त स्वर था उस नाटक में। समय के साथ सामाजिक एवं पारिवारिक परिवेश में बहुत परिवर्तन आ गये, संस्कृति में टेक्नोलॉजी का दखल भी बढ़ता ही जा रहा है, सामाजिक विद्रूपताओं एवं दाम्पत्य जीवन की असमान जटिलताओं को लेकर कोई रचना गढ़ने का संकल्प मेरी चेतना के गर्भ में पल रहा था, तभी एकाएक कम्प्यूटरीकरण सर्वत्र छाने लगा। कम्प्यूटर की शब्दावली में ‘वायरस’ वह प्रक्रिया है जो अगर लग जाये तो उपकरण के सामान्य व्यवहार में उलटफेर कर देती है, अजीब से विकृत और बेतरतीब परिणाम उभरने लगते हैं !
मेरी साहित्यिक संवेदना ऐसे प्रसंगों से मूलत: आबद्ध रही है-‘स्पेयर पार्टस’ ‘बूस्टर चालू आहे’, ‘रिमोट कंट्रोल’, ‘उत्प्रेरक’ ‘क्रैश’ आदि कहानियाँ इसी से प्रवृत्त हैं। साहित्य में जब राजनीति घुसपैठ कर सकती है तो तकनीकी विम्ब क्यों पीछे रहें ? बस लगा कि ऐसी मानवीय विसंगति का ‘वायरस’ किसी घर को भी लग सकता है.......दाम्पत्य जीवन, दिमाग़, विचार, किसी पर कोई क्षण ग्रन्थि या स्थिति वायरस के रूप में आक्रमण कर देते है और परिणाम में जो जद्दोजहद प्रसूत होती है, उसका एक अदना उदाहरण है संलग्न नाटक-‘वायरस’। ‘धक्का पम्प’, ‘व्याकरण’, ‘अन्धकूप’, ‘चिन्दी मास्टर’ एवं ‘चिमनी चोगा’ के बाद लिखे गये नवीनतम नाटक ‘वायरस’ को अपनी प्रिय रचना मानता हूँ......जिन रंगकर्मियों ने इसे पढ़ा,
सभी को विषय-वस्तु एवं उसकी प्रयोगशीलता पसन्द आयी है। रचनाओं के लिए पात्रों को पैदा करना भूत-प्रेतों को जगाने जैसा है। जगाने के बाद उन्हें निभाना होता है, वर्ना विकृत प्रभाव पड़ सकते हैं। ऐसे अनेक भूतप्रेतों से खाली समय में मैं घिर जाता हूँ ! वन्दना और रंजना के चरित्रों का विरोधाभास, विवाह की ज्वलन्त सामाजिक समस्या आदि मुद्दों के कारण यह नि:संदेह एक आम घरेलू कथानक है......किन्तु तकनीकी बिम्ब एवं निदान के लिए सिर उठाते अनोखे उपक्रम का वास्तविक अन्तध्वर्स संपूर्ण स्थिति को नया प्रयोगात्मक आयाम दे पाये-ऐसा मेरा प्रयत्न रहा है।
पुस्तक के अन्त में लघुनाटक ‘धक्का पम्प’ भी यहाँ शामिल है ! सन्’ 75 के आसपास जब नाट्य आन्दोलन करवटें ले रहा था, तब लिखी गयी इस व्यंग्य नाटिका को अज्ञेय जी ने ‘नया-प्रतीक’ में छापा था। फिर इसके कई मंचन हुए। जनवरी ’77 में ये म.प्र. कलापरिषद् के तत्त्वाधान में आयोजित रंगशिविर के ‘छतरियाँ’ ‘अपरिभाषित’ तथा ‘एवं इन्द्रजित’ के साथ ‘धक्का-पम्प’ का निर्देशन श्री एम.के. रैना ने किया था और फिर प्रस्तुति कई शहरों में हुई। इसी तरह उन्हीं दिनों स्व. रमेश बक्षी के आवेश टैरेस थियेटर के तहत दिल्ली में हेमन्त मिश्र के निर्देशन में इसका मंचन हुआ।
‘मंच’ वास्तव में नाटक की सीमाओं का रेखांकन है। उन दिनों नाटक अपनी सीमाओं को तोड़कर दर्शकों के बीच घुल-मिलकर बैठने को लालायित हो रहे थे- ‘धक्का-पम्प’ इसी लालसा का उदाहरण है। इसके माध्यम से युवा वर्ग की अकर्मण्यता, आलस्य और उच्छृंखल प्रवृत्ति पर कुठाराघात के अलावा व्यक्ति और व्यवस्था की जड़ विसंगतियों पर चोट भी की गयी है ! इस पर अंग्रेजी में लिखी गयी एम.के. रैना की मूल टिप्पणी नाटिका के आरम्भ में जोड़ी जा रही है।
पुस्तक के रूप में इन कृतियों के उपलब्ध होने पर रंगकर्मियों की नाट्य संभावानाएँ बलवती होंगी-ऐसी मेरी कामना है।
राजेश जैन
वायरस
पात्र-परिचय
मथुरा प्रसाद : बाप (62 वर्ष)
केसरबाई : मथुरा प्रसाद की पत्नी (55वर्ष)
धीरज : मथुरा प्रसाद का इकलौता पुत्र (35 वर्ष)
रजनी : धीरज की सुन्दर पत्नी (30 वर्ष)
कल्पना : पहली बेटी, विवाहित
रंजना : दूसरी बेटी, विवाहित
वन्दना : तीसरी बेटी, अविवाहित
संवेदना : चौथी बेटी, अविवाहित
अतुल : रंजना का पति, कम्पनी एग्जीक्यूटिव
संजय : कल्पना का पति
विपुल : रंजना-अतुल का पुत्र
अंकिता : रंजना-अतुल की पुत्री
केसरबाई : मथुरा प्रसाद की पत्नी (55वर्ष)
धीरज : मथुरा प्रसाद का इकलौता पुत्र (35 वर्ष)
रजनी : धीरज की सुन्दर पत्नी (30 वर्ष)
कल्पना : पहली बेटी, विवाहित
रंजना : दूसरी बेटी, विवाहित
वन्दना : तीसरी बेटी, अविवाहित
संवेदना : चौथी बेटी, अविवाहित
अतुल : रंजना का पति, कम्पनी एग्जीक्यूटिव
संजय : कल्पना का पति
विपुल : रंजना-अतुल का पुत्र
अंकिता : रंजना-अतुल की पुत्री
दृश्य एक
[स्थान-उच्च मध्यवर्गीय मथुरा प्रसाद का कस्बा स्थित घर....बैठक में तख्त
रखा है। कुछ कुर्सियाँ और टेलीफोन भी....बगल से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हुईं।
दरवाजा अन्दर की ओर खुलता है।
मथुरा प्रसाद के नाम की गुहार लगाकर पोस्टमैन बाहर से ही कुछ चिट्ठियाँ फेंक जाता है। मथुरा प्रसाद और केसबाई का प्रवेश। मथुरा प्रसाद का पैर पत्रों पर पड़ जाता है।]
केसरबाई : अरे ये चिट्ठियाँ आयी हैं और आपने उन पर पैर रख दिया.....!
मथुरा प्रसाद : भूल हो गयी.....(चिट्ठियाँ उठाने लगते हैं।)
केसरबाई : पता नहीं इनमें कौन-सी अच्छी खबर हो और आपका पैर पड़ने से मैली हो जाये ! चिट्ठी को रौंदना अशुभ होता है।
मथुरा प्रसाद : अब शुभ बचा ही क्या है ?
केसरबाई : मन इतना छोटा न करो। भगवान सबकी परीक्षा लेता है और परीक्षा का स्वरूप तथा समय तय नहीं होता.....।
मथुरा प्रसाद : यह भी क्या स्वरूप हुआ ? समय भी निकलता जा रहा है... लड़कियों की उमर बढ़ रही है और हमारी ज़िन्दगी घटती जा रही है। हम हमेशा परीक्षा ही देते रहेंगे ?......यह संसार न हुआ, कोई परीक्षाहाल है जैसे...
(चिट्ठियाँ देखते हैं)
केसरबाई : किसकी हैं ? कहीं से कोई रिश्ते की खबर है क्या ?
मथुरा प्रसाद : वही तो देख रहा हूँ !
केसरबाई : भगवान करे, जैसे रंजना और कल्पना के लिए अतुल और संजय जैसे लड़के मिल गये.....वैसे ही वन्दना और संवेदना के लिए भी मिल जायें.....
मथुरा प्रसाद : तुम तो ऐसे कह रही हो, मानों भगवान के यहाँ भी फ़ोटो कापीइंग मशीन लगी हो.....अतुल और संजय की एक-एक फ़ोटोकापी और निकलवा लोगी.....
मथुरा प्रसाद के नाम की गुहार लगाकर पोस्टमैन बाहर से ही कुछ चिट्ठियाँ फेंक जाता है। मथुरा प्रसाद और केसबाई का प्रवेश। मथुरा प्रसाद का पैर पत्रों पर पड़ जाता है।]
केसरबाई : अरे ये चिट्ठियाँ आयी हैं और आपने उन पर पैर रख दिया.....!
मथुरा प्रसाद : भूल हो गयी.....(चिट्ठियाँ उठाने लगते हैं।)
केसरबाई : पता नहीं इनमें कौन-सी अच्छी खबर हो और आपका पैर पड़ने से मैली हो जाये ! चिट्ठी को रौंदना अशुभ होता है।
मथुरा प्रसाद : अब शुभ बचा ही क्या है ?
केसरबाई : मन इतना छोटा न करो। भगवान सबकी परीक्षा लेता है और परीक्षा का स्वरूप तथा समय तय नहीं होता.....।
मथुरा प्रसाद : यह भी क्या स्वरूप हुआ ? समय भी निकलता जा रहा है... लड़कियों की उमर बढ़ रही है और हमारी ज़िन्दगी घटती जा रही है। हम हमेशा परीक्षा ही देते रहेंगे ?......यह संसार न हुआ, कोई परीक्षाहाल है जैसे...
(चिट्ठियाँ देखते हैं)
केसरबाई : किसकी हैं ? कहीं से कोई रिश्ते की खबर है क्या ?
मथुरा प्रसाद : वही तो देख रहा हूँ !
केसरबाई : भगवान करे, जैसे रंजना और कल्पना के लिए अतुल और संजय जैसे लड़के मिल गये.....वैसे ही वन्दना और संवेदना के लिए भी मिल जायें.....
मथुरा प्रसाद : तुम तो ऐसे कह रही हो, मानों भगवान के यहाँ भी फ़ोटो कापीइंग मशीन लगी हो.....अतुल और संजय की एक-एक फ़ोटोकापी और निकलवा लोगी.....
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book