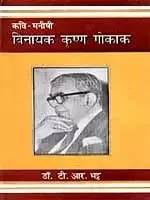|
संस्मरण >> विनायक कृष्ण गोकाक विनायक कृष्ण गोकाकटी. आर. भट्ट
|
58 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है विनायक कृष्ण गोकाक...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
वर्ष 1990 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विनायक कृष्ण गोकाक की
स्वरलहरी ‘कर्णांटिक’ नाद-सौन्दर्य का पंचम स्वर है। इस स्वर
के रस-संचार पिछले छह दशकों से केवल भारतीय साहित्य को ही नहीं बल्कि
विश्व साहित्य को भी निनादित करता है। कन्नड़ में 50 और अंग्रेजी में 25
से अधिक कृतियों के प्रणेता विनायक के काव्य दर्शन में एक विश्व-मानव का
विराट् दर्शन होता है। काव्यर्षि गोकाक की कालजयी रचना ‘भारत सिन्धु
रश्मि’ में काव्य और जीवन का यही सामरस्य परिलक्षित होता है, जिसमें
विश्वरथ के संचालन से अपनी जीवन-यात्रा का प्रारम्भ करने वाला रश्मि सारथी
अन्त में विश्व जनीन भावना से ओतप्रोत विश्वामित्र के रूप में शाश्वत
प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ‘गोकाक’ (गो-काकु) शब्द अपने आप
में स्वर्ग की स्वरलहरी का बोधक है। अर्थ और परमार्थ का साहित्यिक और
सांस्कृति संगम ही विनायक कृष्ण गोकाक का काव्यार्थ है, जिसका एकमात्र
ध्येय है विश्व विजयिनी मानवता के प्रति आस्था का प्रजागरण।
वाङ्मुख
भारतीय ज्ञानपीठ के प्रतीक के रूप में स्वीकृति वाग्देवी चतुर्भज ब्रह्मा
की ह्लादिनी शक्ति है। वाणी, ज्ञान, दर्शन, और शान्ति ही ये चार भुजाएँ
हैं। वाणी प्राणी का लक्षण है। वाणी के माध्यम से ही ज्ञान की प्राप्ति
होती है। सम्यक् ज्ञान सम्यक् दर्शन का सोपान बनता है। वाणी, ज्ञान और
दर्शन के समन्वय से व्यक्ति के भीतर और बाहर शान्ति की प्रतिष्ठा होती है।
वाग्देवी के इसी चतुर्मुख व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर ज्ञान की विलप्ति,
अनुपलब्ध और अप्रकाशित सामग्री के अनुसन्धान और प्रकाशन तथा लोकहितकारी
मौलिक साहित्य के निर्माण के लिए सन् 1944 में भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना
हुई।
ज्ञान-विज्ञान चिन्मय चैतन्य धारा है। यह केवल चिरन्तन और निरन्तर ही नहीं है, बल्कि जिज्ञासु के भीतर संस्कार के अनुरूप प्रकट होने वाली उज्जवल कान्तिधारा भी है। इस धारा को पहचान कर इसके द्रष्टा-स्रष्टा मनीषियों को नमन ज्ञान के प्रत्येक आराधक का कर्तव्य होता है। इसी कर्तव्य को कार्यरूप देने का प्रयास किया है सन् 1965 से प्रवर्तित ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस पुरस्कार की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि भाषा, साहित्य और दर्शन को किसी प्रान्तीय अथवा क्षेत्रीय दृष्टि से न देखकर अखिल भारतीय धरातल पर प्रतिष्ठित करने का भारतीय साहित्य के क्षेत्र में, यह पहला प्रयास था। भारत-भारती की भारतीयता को समन्वित दृष्टि से देखने का यह कार्य आज इतिहास का विषय बन गया है।
भारतीय ज्ञानपीठ ने इस प्रक्रिया के अन्तर्गत अब तक 28 वाङ्मय तपस्वियों का आशीर्वाद प्राप्त किया है। इनमें से 5 कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं।’ ‘रामायण दर्शनम् के यशस्वी लेखक डा० के०वी० पुट्टुप्पा, संसार के समस्त ज्ञान को चार तन्त्रियों में झंकृत करने वाले द० रा० बेन्द्रे, वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध और बहुमुखी प्रतिभाशाली डा० शिवराम कारन्त और ऋषितुल्य लेखक मास्ति वेंकटेश अय्यंगार के पश्चात् ‘भारत-सिन्धुरश्मि’ के परिणतप्रज्ञ लेखक डा० विनायक कृष्ण गोकाक का नाम वाग्देवी के वरदपुत्रों की इस गौरवपूर्ण परम्परा में आ गया है। वास्तव में वर्ष 1990 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विनायक कृष्ण गोकाक की स्वरलहरी ‘कर्णाटिक’ नाद-सौन्दर्य का पंचम स्वर है। इस स्वर का रस-संचार पिछले छह दशकों से केवल भारतीय साहित्य को ही नहीं, बल्कि विश्व-साहित्य को भी निनादित करता रहा है। केवल भारतीय साहित्य को ही नहीं बल्कि विश्व-साहित्य को भी निदादित करता रहा है। कन्नड़ में 50 और अंग्रेज़ी में 25 से अधिक कृतियों के प्रणेता विनायक के काव्य-दर्शन में एक विश्वमानव का विराट् दर्शन होता है। काव्यर्षि गोकाक की कालजयी रचना ‘भारत सिन्धुरश्मि’ में काव्य और जीवन का यही सामरस्य परिलक्षित होता है, जिसमें विश्वरथ संचालन से अपनी जीवन-यात्रा का प्रारम्भ करने वाला रश्मिसारथी अन्त में विश्वजनीन भावना से ओतप्रोत विश्वामित्र के रूप में शाश्वत प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।
‘गोकाक’ (गो-काकु) शब्द अपने आप में स्वर्ग की स्वर-लहरी का बोधक है। अर्थ और परमार्थ का साहित्यिक और सास्कृतिक संगम ही विनायक कृण्ष गोगाक का काव्यार्थ है, जिनका एकमात्र ध्येय है विश्वविजयी मानवता के प्रति आस्था का प्रजागरण।
डा० गोकाक साहित्य के क्षेत्र में जितने विख्यात हैं, प्रशासन, शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में भी उतने ही प्रतिष्ठित हैं। साहित्य के आचार्य के रूप में देश-विदेश के कई विश्वविद्यालय से उनका सम्बन्ध रहा है और लगभग आधी शताब्दी तक शिक्षा और प्रशासन के कई पदों को उन्होंने अलंकृत किया। लगभग प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में काम करना एक बात है और एक विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित करना एकदम अनोखी बात है। इसी दुष्कर कार्य को प्रो० गोकाक ने सुकर बनाया। इस शताब्दी के अवतार-पुरुष श्री सत्य साई बाबा ने प्रशान्तनिलय में उच्च विद्या के प्रचार-प्रसार के लिए विश्वविद्यालय के स्तर की एक संस्था स्थापित करने की बात सोची, तो बाबा के इस संकल्प को सक्रिय रूप प्रो० गोकाक ने दिया। सन्मनुष्यता के समर्थक और समरसरता के संस्थापक बाबा के मन में प्रथम मानवता को जो महिमामय आदर्श परिकल्पित था, उसे इसी अवधि में गोकाक के कृतित्व में सहज रूप से दार्शनिकता और आध्यात्मिकता का समावेश हुआ। यही समय था जब ‘समरसवे जीवन’ नाम का उनका बृहद उपन्यास चार खण्डों में पूरा हुआ था। जिसका अन्तिम खण्ड ‘नरहरि’ ‘अवतार’ और विभूति अद्भुत सामंजस्य प्रस्तुत करता है। ‘नरहरि’ शब्द में ही भव्यता और दिव्यता का सामंजस्य व्यंजित होता है। नर को हरि के स्तर तक ऊपर उठाया और इस प्रक्रिया में हरि को नर के समीप लाना आर्ष कवि का आदर्श होता है और इसी आदर्श को ध्यान में रखकर काव्यर्षि गोकाक ने ‘भारत-सिन्धुरश्मि शीर्षक महाकाव्य की परिकल्पना की।
कवि गोकाक की आध्यामिक चेतना का बीज उनकी प्रारम्भिक रचना ‘कलोपासक’ में ही परिलक्षित हो जाता है। कला की यह उपासना कवि को धरती और स्वर्ग के बीच तादाम्त्य सथापित करने की ओर प्रेरित करती है। इसी प्रेरणा का सुखद परिणाम है-‘‘द्यावा-पृथ्वी’ की रचना, सत्य के द्रष्टा और सारस्वत संसार के स्रष्टा शेक्सपियर ने इस सत्य को धरती और स्वर्ग के बीच संचरित होनेवाले कवि के नेत्रों में देखा था। इसी प्रकार कवि-मनीषी गोकाक ने द्यावा और पृथिवी के समस्त भाव को सरस कविता का रूप दिया है। ‘द्यावा-पृथिवी’ की रचना के पीछे श्रुतिमाता की एक सूक्ति पग-पग पर अपनी प्रतिध्वनि सुनाती दिखाई देती है –
ज्ञान-विज्ञान चिन्मय चैतन्य धारा है। यह केवल चिरन्तन और निरन्तर ही नहीं है, बल्कि जिज्ञासु के भीतर संस्कार के अनुरूप प्रकट होने वाली उज्जवल कान्तिधारा भी है। इस धारा को पहचान कर इसके द्रष्टा-स्रष्टा मनीषियों को नमन ज्ञान के प्रत्येक आराधक का कर्तव्य होता है। इसी कर्तव्य को कार्यरूप देने का प्रयास किया है सन् 1965 से प्रवर्तित ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस पुरस्कार की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि भाषा, साहित्य और दर्शन को किसी प्रान्तीय अथवा क्षेत्रीय दृष्टि से न देखकर अखिल भारतीय धरातल पर प्रतिष्ठित करने का भारतीय साहित्य के क्षेत्र में, यह पहला प्रयास था। भारत-भारती की भारतीयता को समन्वित दृष्टि से देखने का यह कार्य आज इतिहास का विषय बन गया है।
भारतीय ज्ञानपीठ ने इस प्रक्रिया के अन्तर्गत अब तक 28 वाङ्मय तपस्वियों का आशीर्वाद प्राप्त किया है। इनमें से 5 कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं।’ ‘रामायण दर्शनम् के यशस्वी लेखक डा० के०वी० पुट्टुप्पा, संसार के समस्त ज्ञान को चार तन्त्रियों में झंकृत करने वाले द० रा० बेन्द्रे, वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध और बहुमुखी प्रतिभाशाली डा० शिवराम कारन्त और ऋषितुल्य लेखक मास्ति वेंकटेश अय्यंगार के पश्चात् ‘भारत-सिन्धुरश्मि’ के परिणतप्रज्ञ लेखक डा० विनायक कृष्ण गोकाक का नाम वाग्देवी के वरदपुत्रों की इस गौरवपूर्ण परम्परा में आ गया है। वास्तव में वर्ष 1990 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विनायक कृष्ण गोकाक की स्वरलहरी ‘कर्णाटिक’ नाद-सौन्दर्य का पंचम स्वर है। इस स्वर का रस-संचार पिछले छह दशकों से केवल भारतीय साहित्य को ही नहीं, बल्कि विश्व-साहित्य को भी निनादित करता रहा है। केवल भारतीय साहित्य को ही नहीं बल्कि विश्व-साहित्य को भी निदादित करता रहा है। कन्नड़ में 50 और अंग्रेज़ी में 25 से अधिक कृतियों के प्रणेता विनायक के काव्य-दर्शन में एक विश्वमानव का विराट् दर्शन होता है। काव्यर्षि गोकाक की कालजयी रचना ‘भारत सिन्धुरश्मि’ में काव्य और जीवन का यही सामरस्य परिलक्षित होता है, जिसमें विश्वरथ संचालन से अपनी जीवन-यात्रा का प्रारम्भ करने वाला रश्मिसारथी अन्त में विश्वजनीन भावना से ओतप्रोत विश्वामित्र के रूप में शाश्वत प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।
‘गोकाक’ (गो-काकु) शब्द अपने आप में स्वर्ग की स्वर-लहरी का बोधक है। अर्थ और परमार्थ का साहित्यिक और सास्कृतिक संगम ही विनायक कृण्ष गोगाक का काव्यार्थ है, जिनका एकमात्र ध्येय है विश्वविजयी मानवता के प्रति आस्था का प्रजागरण।
डा० गोकाक साहित्य के क्षेत्र में जितने विख्यात हैं, प्रशासन, शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में भी उतने ही प्रतिष्ठित हैं। साहित्य के आचार्य के रूप में देश-विदेश के कई विश्वविद्यालय से उनका सम्बन्ध रहा है और लगभग आधी शताब्दी तक शिक्षा और प्रशासन के कई पदों को उन्होंने अलंकृत किया। लगभग प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में काम करना एक बात है और एक विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित करना एकदम अनोखी बात है। इसी दुष्कर कार्य को प्रो० गोकाक ने सुकर बनाया। इस शताब्दी के अवतार-पुरुष श्री सत्य साई बाबा ने प्रशान्तनिलय में उच्च विद्या के प्रचार-प्रसार के लिए विश्वविद्यालय के स्तर की एक संस्था स्थापित करने की बात सोची, तो बाबा के इस संकल्प को सक्रिय रूप प्रो० गोकाक ने दिया। सन्मनुष्यता के समर्थक और समरसरता के संस्थापक बाबा के मन में प्रथम मानवता को जो महिमामय आदर्श परिकल्पित था, उसे इसी अवधि में गोकाक के कृतित्व में सहज रूप से दार्शनिकता और आध्यात्मिकता का समावेश हुआ। यही समय था जब ‘समरसवे जीवन’ नाम का उनका बृहद उपन्यास चार खण्डों में पूरा हुआ था। जिसका अन्तिम खण्ड ‘नरहरि’ ‘अवतार’ और विभूति अद्भुत सामंजस्य प्रस्तुत करता है। ‘नरहरि’ शब्द में ही भव्यता और दिव्यता का सामंजस्य व्यंजित होता है। नर को हरि के स्तर तक ऊपर उठाया और इस प्रक्रिया में हरि को नर के समीप लाना आर्ष कवि का आदर्श होता है और इसी आदर्श को ध्यान में रखकर काव्यर्षि गोकाक ने ‘भारत-सिन्धुरश्मि शीर्षक महाकाव्य की परिकल्पना की।
कवि गोकाक की आध्यामिक चेतना का बीज उनकी प्रारम्भिक रचना ‘कलोपासक’ में ही परिलक्षित हो जाता है। कला की यह उपासना कवि को धरती और स्वर्ग के बीच तादाम्त्य सथापित करने की ओर प्रेरित करती है। इसी प्रेरणा का सुखद परिणाम है-‘‘द्यावा-पृथ्वी’ की रचना, सत्य के द्रष्टा और सारस्वत संसार के स्रष्टा शेक्सपियर ने इस सत्य को धरती और स्वर्ग के बीच संचरित होनेवाले कवि के नेत्रों में देखा था। इसी प्रकार कवि-मनीषी गोकाक ने द्यावा और पृथिवी के समस्त भाव को सरस कविता का रूप दिया है। ‘द्यावा-पृथिवी’ की रचना के पीछे श्रुतिमाता की एक सूक्ति पग-पग पर अपनी प्रतिध्वनि सुनाती दिखाई देती है –
इदम द्यावा-पृथिवी सत्यमस्तु। पितर्मातर्यदिहोपब्रु वेमां।
भूतं देवानामवमे अवोभिः विद्यामेषं जीरदानुम्।।
भूतं देवानामवमे अवोभिः विद्यामेषं जीरदानुम्।।
जिस कवि के लिए धरती माता है और प्रकाश पिता का प्रतीक है उसे धूल में भी
दिखाई देते हैं। धरती और आकाश के इसी सहज सम्पर्क के कारण सागर की लहरें
बादल में भाप बनकर तपती धरती को शीतलता प्रदान करती हैं। एक ही रस-तत्व के
इस रूपान्तरण को देखकर गोकाक का कवि-हृदय कहता है:
रूप का यह अन्तरण
अद्भुत आश्चर्यजनक इन्द्रजाल
मृत्तिका बन जाती है
मत्युंजय की जटा,
धूल देवता बनती है
गीली मिट्टी बनती है नीला आकाश
मुठ्ठी भर धूल।
पर आँख खुल जाती है तो
अम्बर दिख जाता है
नारसिंह अधरों को
विस्फारित करती है
विश्वों का स्वास्तिपाठ
उच्चारित करती है
सातो संसार के आर-पार घेर कर
सरजाती संसृति को
धूल धवल मुट्ठी भर।
अद्भुत आश्चर्यजनक इन्द्रजाल
मृत्तिका बन जाती है
मत्युंजय की जटा,
धूल देवता बनती है
गीली मिट्टी बनती है नीला आकाश
मुठ्ठी भर धूल।
पर आँख खुल जाती है तो
अम्बर दिख जाता है
नारसिंह अधरों को
विस्फारित करती है
विश्वों का स्वास्तिपाठ
उच्चारित करती है
सातो संसार के आर-पार घेर कर
सरजाती संसृति को
धूल धवल मुट्ठी भर।
कवि गोकाक की काव्य-साधना इसी आध्यात्मिक चेतना को अपना सम्बल
बनाकर
आगे बढ़ती है। ऋग्वेद की विनम्रता, यजुर्वेद की धारणा, सामवेद की
समरसता-तीनों को आत्मसात् करने में जब कवि गोकाक सफल होता है, तब
‘भारत-सिन्धुरश्मि’ का प्रादुर्भाव होता है। जिस
प्रकार
पृथ्वी और स्वर्ग में कोई अन्तर नहीं है, उसी प्रकार नर और नारायण में भी
कोई अन्तर नहीं है। नर में ही नारायण का निवास है। यही तथ्य
‘भारत-सिन्धुरश्मि’ का काव्यात्मक सत्य है। सिन्धु
शब्द जीवन
की अजस्र रसधारा का द्योतक है, तो रश्मि जीवन के परमार्थ को आलोकित करने
वाली कान्तिमाला है। जल ही प्रकाश को जन्म देता है और प्रकाश से ही जल
प्रवाहित होता है। वेद का प्रमाण है।–आपो
ज्योतिरसोमृतम्’
पानी ही प्रकाश है, वही रस है, वही अमृत है। यही समीकरण
‘भारत-सिन्धुरश्मि’ के बारह काण्डों में सजग
अभिव्यक्ति पाता
है।
अपनी सर्वोत्कृष्ट रचना ‘भारत-सिन्धुरश्मि’ में कवि गोकाक ने गायत्री मन्त्र के द्रष्टा विश्वामित्र को प्रमुख पात्र बनाकर अपने काव्य-दर्शन का बहुत ही गहरा परिचय दिया है। वैदिक चिन्तन में विश्वामित्र का एक विशिष्ट स्थान है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के शब्दों में विश्वामित्र विद्या, तपस्या, प्रेम और कारुण्य के मूर्त रूप हैं। जीवकारुण्य की भावना से समस्त जीवजगत् को सहृदयता के साथ आत्मसात् करते-करते विश्वरथ अन्त में विश्वामित्र का रूप धारण करता है, ‘रश्मि’ काव्य के अन्त में महाकाल के साथ महातपस्वी विश्वामित्र का जो संवाद है, वही सम्भवता कवि गोकाक का सन्देश है।
माया-कल्पित देश-काल की जनयित्री धरती माता की ममता के मोह में अपने को कृतकृत्य समझने वाला महाकाल महामनस्वी विश्वामित्र से पूछता है कि क्या यह भोली-भाली धरती आनन्द-सागर में निक्षिप्त निसर्ग आनन्द को पहचान पाती है।
विश्वामित्र का वाङ्मय मौन इस प्रहेलिका का समाधान प्रस्तुत करते हुए कहता है कि संसार का समस्त ज्ञान मानव की मधुर मनोहारिता से परिचित प्राणिमात्र के पाणि-तल में विद्यमान है। इस करतलगत अमलक का रसास्वादन करने का सौभाग्य जिस सुकृति को मिलता है, उसके तरल तपस्वी नयनों से सारा विवेक झलकता है और नीलनयन की कमनीयता में नीलगगन की रमणीयता निर्भय, निर्मम, निर्द्वन्द्व और निर्लिप्ति निर्वेद का अनुभव करती है। यही कवि गोकाक का आत्मवेद है जो भारत-सिन्धुरश्मि’ में काव्य बनकर अवतरित होता है। विश्वामित्र का महाप्रस्थान पार्थिव जगत् का परित्याग नहीं है, केवल पार्थिव शरीर का विसर्जन है। आत्मा का अनाहद नाद सारे विश्व को अखंड आनन्द का निलय बना देता है। अनन्त आकाश की प्राण-नाड़ी में एक बार फिर स्पन्दन पैदा हो जाता है। सारा विश्व मैत्री से परिपूर्ण बन जाता है। विश्वरथ विश्वामित्र बन जाता है। आज फिर इस विश्वामित्र की आवश्यकता महसूस करने वाले महाकवि इस काव्य के उपसंहार में यही मंगलकामना प्रकट करते हैं कि आज फिर विश्वामित्र विश्व में अवतरित हो।
अपनी सर्वोत्कृष्ट रचना ‘भारत-सिन्धुरश्मि’ में कवि गोकाक ने गायत्री मन्त्र के द्रष्टा विश्वामित्र को प्रमुख पात्र बनाकर अपने काव्य-दर्शन का बहुत ही गहरा परिचय दिया है। वैदिक चिन्तन में विश्वामित्र का एक विशिष्ट स्थान है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के शब्दों में विश्वामित्र विद्या, तपस्या, प्रेम और कारुण्य के मूर्त रूप हैं। जीवकारुण्य की भावना से समस्त जीवजगत् को सहृदयता के साथ आत्मसात् करते-करते विश्वरथ अन्त में विश्वामित्र का रूप धारण करता है, ‘रश्मि’ काव्य के अन्त में महाकाल के साथ महातपस्वी विश्वामित्र का जो संवाद है, वही सम्भवता कवि गोकाक का सन्देश है।
माया-कल्पित देश-काल की जनयित्री धरती माता की ममता के मोह में अपने को कृतकृत्य समझने वाला महाकाल महामनस्वी विश्वामित्र से पूछता है कि क्या यह भोली-भाली धरती आनन्द-सागर में निक्षिप्त निसर्ग आनन्द को पहचान पाती है।
विश्वामित्र का वाङ्मय मौन इस प्रहेलिका का समाधान प्रस्तुत करते हुए कहता है कि संसार का समस्त ज्ञान मानव की मधुर मनोहारिता से परिचित प्राणिमात्र के पाणि-तल में विद्यमान है। इस करतलगत अमलक का रसास्वादन करने का सौभाग्य जिस सुकृति को मिलता है, उसके तरल तपस्वी नयनों से सारा विवेक झलकता है और नीलनयन की कमनीयता में नीलगगन की रमणीयता निर्भय, निर्मम, निर्द्वन्द्व और निर्लिप्ति निर्वेद का अनुभव करती है। यही कवि गोकाक का आत्मवेद है जो भारत-सिन्धुरश्मि’ में काव्य बनकर अवतरित होता है। विश्वामित्र का महाप्रस्थान पार्थिव जगत् का परित्याग नहीं है, केवल पार्थिव शरीर का विसर्जन है। आत्मा का अनाहद नाद सारे विश्व को अखंड आनन्द का निलय बना देता है। अनन्त आकाश की प्राण-नाड़ी में एक बार फिर स्पन्दन पैदा हो जाता है। सारा विश्व मैत्री से परिपूर्ण बन जाता है। विश्वरथ विश्वामित्र बन जाता है। आज फिर इस विश्वामित्र की आवश्यकता महसूस करने वाले महाकवि इस काव्य के उपसंहार में यही मंगलकामना प्रकट करते हैं कि आज फिर विश्वामित्र विश्व में अवतरित हो।
लोक-कल्याण के संधाता और
सृष्टि-सौन्दर्य के उद्गाता
विश्व-मानवता के अधिनेता
वे फिर अपनी
सात धाराओं और मालाओं को लेकर
विश्वात्मा के विराट् सदन की ओर
अभियान करें-
मानव दिव्य जीनव का पात्र बने
मानवता की जय हो
प्रणवनाद प्राणों का प्रणयन करता रहे।
सृष्टि-सौन्दर्य के उद्गाता
विश्व-मानवता के अधिनेता
वे फिर अपनी
सात धाराओं और मालाओं को लेकर
विश्वात्मा के विराट् सदन की ओर
अभियान करें-
मानव दिव्य जीनव का पात्र बने
मानवता की जय हो
प्रणवनाद प्राणों का प्रणयन करता रहे।
इतना कहने और करने पर भी कवि अपने को ठीक-ठीक समझ नहीं पाता। उसे यह बात
समझ में नहीं आती है कि आखिर गोकाक नाम का व्यक्ति कौन है। क्या यह गोकाक
है जिसको लोग गोकाक मानते हैं, या इन दोनों से अलग एक अन्य गोकाक है जो
वास्तव में अनन्य गोकाक है। इस विचिकित्सा में कवि स्वयं बह जाता है और कह
देता है कि यदि किसी प्रकार से ये तीनों गोकाक एक बन जाएँ तो फिर उस गोकाक
के लिए न नाम की आवश्यकता है। न रूप की और न कविता की। इस मधुमती भूमिका
में मधुमय बन जाता है और वही मधुराक्षर काव्य का मंलगमय रूप धारण करता है।
यह एक ऐसी विशिष्ट, विचित्र और विलक्षण भाव-भूमिका है, जो कवि को ऋषिकेस
स्तर पर पहुँचा देती है जहाँ पर सब कुछ सुन्दर है। यह सौन्दर्य भोग में
नहीं, त्याग में है, राग में नहीं, वैराग्य में है इसी भूमिका को
:‘भारत-सिन्धुरश्मि की भूमिका का अन्तिम उद्गार एक सुन्दर
संज्ञा
देता है वह है -‘वैराग्य सौन्दर्य’।।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book