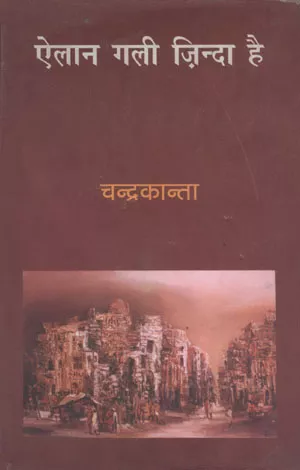|
कहानी संग्रह >> सूरज उगने तक सूरज उगने तकचन्द्रकान्ता
|
188 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है सूरज उगने तक.....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
मैक्सिम गोर्की ने एक बार रोम्या रोलां के नाम अपने पत्र में एक चिंता
व्यक्त की थी कि हम बड़े-बूढ़े लोग जो जल्दी ही इस दुनिया से कूच कर
जाएँगे, अपने पीछे बच्चों के लिए एक दुःखद बपौती छोड़ जाएंगे, एक उदास
ज़िन्दगी उन्हें वसीयत के रुप में सौंपेंगे ....जबकि वे चाहते थे कि हमारे
बाद इस पृथ्वी को हमसे बेहतर योग्य और प्रतिभाशाली लोग आबाद कर सकें। ऐसी
ही चिंता शायद हर प्रतिबद्ध रचनाकार की होती है, भविष्य की चिन्ता। तभी तो
साहित्य को वह इंसानी जीवन की शर्त मानता है, समय का जीवंत साक्ष्य
प्रस्तुत करते हुए अपनी एक्सरे नज़रों से सही-गलत की छानबीन करता है
स्थितियों घटनाओं को उठाकर विभिन्न परिवेश में अवस्था से जूझते पात्रों की
मनोव्यथा का आकलन करता है।
कश्मीर में जन्मी हिन्दी की प्रगतिशील लेखिका चन्द्रकान्ता का भी अपने लेखन के पीछे कुछ ऐसा ही भाव रहा है। उनकी कहानियों में जहाँ एक ओर आपसी प्रेम और सौहार्द की बेमिसाल धरती कश्मीर और पंजाब का लहूलुहान चेहरा है। घरों से निष्कासन और अपने ही देश में विदेशी होने की पीड़ा है। वहीं आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के दोगलेपन में फँसे आम आदमी की व्याथा भी है; कहीं भौतिक समृद्धि और औद्योगिक प्रगति के बहाने मशीनी ज़िन्दगी के चक्रव्यूह से घिरे आदमी की छटपटाहट है तो कहीं मानवीय रिश्तों की ठण्डी कब्रों में क़ैद होकर निःशेष होने की पीड़ा है। इसके बावजूद व्यक्ति की भीतरी ऊर्जा और संघर्ष की शक्ति में अदम्य विश्वास भी है। तभी तो लेखिका निकेनार पारा की तरह आवाज़ पैदा करना चाहती है, बोलती है कि वे लोग भी बोलना सीखें जो चुप रहते हैं। ग़लत का मौन-स्वीकार संघर्ष-विमुखता है अतः आवाज़ उठाना ज़रूरी है।
रचनाकार अपनी अनुभव-सम्पन्नता के माध्यम से संवेदनात्मक धरातल पर पाठक के सोच पर दस्तक देती है। क्योंकि गोर्की की तरह उसके मन में भी एक बेहतर भविष्य का सपना पल रहा है। आशा है, अपने आप को, अपने समय को जानने, समझने और सँवारने की चाहत लिये इन कहानियों को पाठक गहराई के साथ पढ़ेंगे और भावनात्मक सुथरेपन से इन्हें महसूस करेंगे।
कश्मीर में जन्मी हिन्दी की प्रगतिशील लेखिका चन्द्रकान्ता का भी अपने लेखन के पीछे कुछ ऐसा ही भाव रहा है। उनकी कहानियों में जहाँ एक ओर आपसी प्रेम और सौहार्द की बेमिसाल धरती कश्मीर और पंजाब का लहूलुहान चेहरा है। घरों से निष्कासन और अपने ही देश में विदेशी होने की पीड़ा है। वहीं आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के दोगलेपन में फँसे आम आदमी की व्याथा भी है; कहीं भौतिक समृद्धि और औद्योगिक प्रगति के बहाने मशीनी ज़िन्दगी के चक्रव्यूह से घिरे आदमी की छटपटाहट है तो कहीं मानवीय रिश्तों की ठण्डी कब्रों में क़ैद होकर निःशेष होने की पीड़ा है। इसके बावजूद व्यक्ति की भीतरी ऊर्जा और संघर्ष की शक्ति में अदम्य विश्वास भी है। तभी तो लेखिका निकेनार पारा की तरह आवाज़ पैदा करना चाहती है, बोलती है कि वे लोग भी बोलना सीखें जो चुप रहते हैं। ग़लत का मौन-स्वीकार संघर्ष-विमुखता है अतः आवाज़ उठाना ज़रूरी है।
रचनाकार अपनी अनुभव-सम्पन्नता के माध्यम से संवेदनात्मक धरातल पर पाठक के सोच पर दस्तक देती है। क्योंकि गोर्की की तरह उसके मन में भी एक बेहतर भविष्य का सपना पल रहा है। आशा है, अपने आप को, अपने समय को जानने, समझने और सँवारने की चाहत लिये इन कहानियों को पाठक गहराई के साथ पढ़ेंगे और भावनात्मक सुथरेपन से इन्हें महसूस करेंगे।
अपने बारे में
अपने बारे में सोचते हुए जब भी मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एक छह-सात वर्ष
की खिलन्दड़ी बच्ची आड़ी–मेड़ी घसीली पगडण्डियों पर हवा से होड़
लेते भागती नज़र आती है। कन्धे तक लटकते बेतरतीब उलझे बाल, मुँह माथे पर
छितराये वह कच्ची दूबिया पगडण्डियों पर ऊँचे चीड़, देवदारों से बतियाती
बेहताशा दौड़ी जा रही है, अकेली-अकेली। जबकि उसके भाई-बहन सम्भ्रान्त घर
के तौर-तरीक़ो के अनुसार घर में बैठे खिलौनों से खेल रह होते हैं।
अकसर किसी बादाम, नाशपाती या अखरोट के पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ती-गिराती अधकुतरे मीठे फल फ्रॉक के घेर में इकट्ठा करती, चीड़ की कटी-टहनियां बटोरती, यह लड़की हाँफती, पसीना-पसीना हुई पहाड़ी पर बने बँगलों में दाखिल हो जाती है, जहाँ एक हाल नुमा हवादार कमरे में तीमारदारों से घिरी एक औरत पलंग पर लेटी होती है। बच्ची बड़े एहतियात से चीड़ की टहनियाँ उसके सिरहाने सजा देती है। डाक्टरों ने जो उस स्त्री को शुद्ध हवा सेवन के लिए शहर के पंचमंज़िला घर से वुरपश गाँव के इस छोटे से बँगलें में रहने के लिए सलाह दी है। अधकुतरे मीठे बादाम, अखरोट जबरदस्ती स्त्री के मुँह में भरने पर लड़की डाँट खाती है पर सिर झटककर हँस देती है। क्योंकि उसके मन में अखण्ड विश्वास है यह तपेदिक की मरीज औरत, जिसकी भूख और उम्र तेज़ी से घट रही है, जो इंच-दर-इंच मौत के करीब खिसकती जा रही है, उसके चुन-चुन कर लाए फल–फूल और चीड़ की कटी टहनियों में जीवन की संजीवनी से जी उठेगी। यह औरत, जो उसकी मां है, मौत के बिस्तर पर भी चिन्तित है कि उसकी इस ‘कलन्दर’ बेटी का क्या होगा ? क्या इसलिए कि लड़की घर के सम्भ्रान्त अनुशासनों में बँध नहीं पाती, लीक तोड़कर चलना चाहती है ?
और जब एक दिन चीड़-देवदार की शफ्फाक हवाओं की गोद में भी वह पलंग खाली हो गया तो वह छः सात वर्ष की चहचहाती बालिका सुग्गे, गुगी और पोशनूल से बतियाना भूल, उम्र से पहले ही बड़ी हो गयी। चुप गुमसुम और अपने भीतर तेजी से कुछ घटने लगा। चीज़ें अपनी शक्लें बदलने लगीं। आकाश का नीला विस्तार एक दमघोंट खोह में क़ैद हो गया। आसमान को अपने पैरों तले तौलने वाले रंगीन पाँखी उसकी नज़रों से दूर चले गये। उसके बाद वह लड़की कभी उन खुली पगडण्डियों पर नहीं दौड़ी उसके भीतर उगमती बेइन्तहा बातें, कौतुक भरे प्रश्न जमकर ग्लेशियर बनते गये। वह बहन-भाई पिता-किसी से भी अपने भीतर उगते बेसिर-पैर के प्रश्न नहीं पूछ पाई। उसने ‘ढंग से’ बात करना, कहना, सीखा ही कहाँ था। तब बारह वर्ष की उम्र में उसने पहली कविता लिखी-‘भर आता जब यह मौन हृदय....’’ क्या भीतर जो घट रहा था उसे जानने के लिए ? ज़रूर यह छुई-मुई उम्र की भावुक अभिव्यक्ति थी, पर महत्त्वपूर्ण इसलिए कि वे पहले-पहले शब्द थे जो मेरे भीतर से पहाड़ी झरने की तरह फटे थे। और उन्हें अपने घरवालों से छिप कर मैंने कागज पर उतारा था। मेरे रचनाकार के जन्म की शुरूआत वही थी। इसलिए मैं आज भी मानती हूँ रचनाकार का जन्म दुख से होता है।
घटनाएँ जीवन में बहुत घटीं, उनका प्रभाव भी मुझ पर पड़ा, पर सभी के साथ घटनाएं घटती हैं। हमारे व्यक्तित्व में कुछ भी जोड़-तोड़ करती हैं। एक घटना, जिसने बचपन को लाँघकर मुझे एकदम ढेर सारे दायित्वों के बीच खड़ा कर बड़ा बना दिया-बहुत छोटी उम्र में पिता की देहरी छोड़नी थी। हमारे विद्वान पिता, प्रोफ़ेसर रामचन्द्र पण्डित ने नारी शिक्षा के हिमायती होने के बावजूद, हम दोनों बहनों के लिए घर और वर समय से पहले ही जुटा लिए। तमाम दानिशमन्दी के बावजूद वे तेजी से बढ़ती अपनी वय से शायद आशंकित थे। उनकी आशंका अपनी जगह सही भी थी, बिना माँ की बेटियों के भविष्य के लिए मेरे लिए यह दूसरा धक्का था, क्योंकि नये घर में तमाम प्यार और आदर की हक़दार होने के बावजूद मुझे लगा कि किसी ने बढ़ी बेदर्दी से आकाश में उड़ान भरते पाँखी के पंख कतर दिये हैं और उसे सोने के पिजड़े में कैद कर दिया है, जो अब उम्र क़ैद है, साल भर इस कैद में आसूं बहाते मैं यह समझ गयी कि क़ैदें ज़िन्दगी की ज़रूरी शर्तें हैं, पर मन में एक ढीठ निश्चय ही उभरता गया कि मेरा मन आसमान की ऊँचाइयाँ छूता रहा है। मैं छोटी उम्र में ही बेहतर कल्पनाशील बन गयी। कुछ करने और बनने की जिद मुझे अक्सर बेचैन रखती। ज़रूर मेरे पति डाक्टर विशिन ने जो तब स्वयं बी.एस.सी के छात्र थे और मेरे ससुराल वालों ने, मेरी कुछ बनने और पाने की ज़िद को समझा और मेरे रास्ते में रुकावटे नहीं डालीं। इसलिए तमाम पारस्परिक मान्यताओं व संहिताओं बीच मैं घर की बड़ी बहू एक बेटी की तरह घर में रही, स्कूल कॉलेज में अपना अध्ययन-मनन ज़ारी रखा।
समय को तो बीतना ही होता है। मैं छिटपुट कविताएं स्कूल-कॉलेज की पत्रिकाओं में लिखती रही। श्रीनगर में गर्ल्स कॉलेज में, फिर गाँधी मेमोरियल कॉलेज में कुछ कविताएं-कुछ कहानियाँ छपीं। एम.ए. करते समय, बिरला कॉलेज पिलानी में एक बार हमारे प्रिंसिपल डॉ. कन्हैयालाल सहल ने कविता प्रतियोगिता के लिए मुझसे एक कविता लिखवायी, जो बाद में पुरस्कृत भी हुई। उस बार पिलानी के विरला ऑडियाटोरियम में पुरस्कार वितरण समारोह में डॉ. सहल ने निरन्तर लिखने और लेखन के उत्तरोत्तर विकास सम्बन्धी जो बातें मुझसे कहीं उनसे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। पिलानी में दो वर्ष अध्यापन करने के बाद मैं अपने पति डॉ. विशिन के साथ हैदराबाद चली गयी। वहींसे मेरा नियमित लेखन आरम्भ हुआ। मैंने नौकरी छोड़कर स्वतन्त्र लेखन का दायित्व उठा लिया। मुझसे नौकरी, लेखक और गृहस्थी साथ-साथ नहीं निभे। चुनाव मेरा अपना था। मेरे पति ने मेरे रास्ते में कभी कोई बाधा नहीं डाली।
सितम्बर 1967 में कल्पना (हैदराबाद) में मेरी पहली कहानी ‘खून के रेशे’ प्रकाशित हुई। उसी वर्ष अक्टूबर में नयी कहानियाँ’ में ‘कैक्टस’ और अगले वर्ष ‘ज्ञानोदय’ में ‘सलाखों के पीछे’’ आदि कहानियाँ प्रकाशित हुई। बाद में धीरे-धीरे अन्य व्यावसायिक-अव्यावसायिक पत्रिकाओं में बराबर लिखती रही। जिस दौर में मैंने नियमित लेखन शुरू किया कथा-जगत में वह दौर काफी बहस-मुबाहसों एवं नये प्रयोगों का दौर था।
नयी कहानी के विरोध में ‘अकहानी’ का नारा बुलन्द किया जा रहा था और कामूकाफ्का की भौंड़ी नकल के फलस्वरूप ‘सन्त्रास’ और सेक्स’ फ़ैशन बनाकर भुनाया जा रहा था। नयी कहानी वाले दौर की तरह ही अनकही के लेखक अपने पूर्ववर्ती लेखकों को अस्वीकार करने लगे थे। उन दिनों अमृतराय ‘नयी कहानियाँ’ का सम्पादन करते थे और मैं बराबर उसमें लिख रही थी। अमृत जी ने ‘‘सार्थक विद्रोह, दशा-दिशा-संभावना’ नाम से एक लेखमाला में ‘सार्थक कहानी’ पर एक बहस की शुरूआत की जिसमें छद्म आधुनिकता का विरोध किया गया और लेखन को समकालीन जीवन एवं भोगे हुए यथार्थ से जोड़कर जीवनास्था पर बल दिया गया मुझे ‘नयी कहानियाँ’ के इस स्तम्भ ने दिशा दी, यह मैं आज भी मानती हूँ।
उसके बाद कहानी सचेतन सामान्तर, जनवादी आदि खेमों में बाँटी गयी। अलग-अलग खेमों अलग-अलग अलमबदार और आलोचक बन गये। पर खेमों ने मुझे कभी आकर्षित नहीं किया। मैं बराबर लिखती रही और अपने लेखन को सँवारती रही। साहित्य पुराना, परम्परावादी या रूढ़ हो सकता है, यह बात आज भी मैं नहीं मानती। समय के इस दस्तावेज को समय के सन्दर्भों के साथ जोड़कर देखने पर भी यह बात स्पष्ट है कि साहित्यकार समय की सीमा के पार देखता और सोचता है। मानवीय संवेगों और स्थितियों से सम्बन्ध रखने के कारण युगों तक हमें अपने भीतर झांकने, सीखने और जीने की प्रेरणा देता है। वह चाहे कथा सरित्सागर, उपनिषद कथाएँ, चन्द्रकान्ता सन्तति हो या तुलसी, कबीर, कालिदास, प्रेमचन्द की रचनाएं हों। साहित्य जीवन की मूलभूत शर्तों से जुड़ा होने के कारण पुराना पड़ नहीं सकता। तभी तो हम टाल्सटाय, गोर्खी, चेखव, दास्तोएवस्की हेमिंग्वे, कालिदास आदि को आज भी बड़े चाव और उत्सुकता से पढ़ते हैं।
नयी कहानी के दौर वालों वालों ने अज्ञेय जैनेन्द्र आदि का विरोध किया तो अनकही वाले खेमे ने साठोत्तरी लेखन से नयी कहानी के रचनाकारों को खारिज कर दिया। दरअसल विरोध की यह नीति ही ग़लत थी। तुलसी, प्रेमचन्द, उग्र, जैनेन्द्र, अज्ञेय, मुक्ति, बोध, राकेश, धर्मवीर, भारती, राजेन्द्र यादव, भीष्म साहनी हमारी अगली पीढ़ियाँ गर्व करेंगी। मैं तब भी मानती थी और आज भी मानती हूँ कि साहित्यकार प्रगतिशील ही होता है। दकियानूसी, वक्त की धार से कटा हुआ कोई भी रचनाकार जीवन के विशाल फलक को खुली आँखों और खुले मन से दूर तक देख नहीं सकता। अतीत, वर्तमान और आगत के चेहरों को पढ़ कर उन्हें सँवारने का स्वप्न देख नहीं सकता। मेरे विचार में जो रचना आम जन के दुःख-सुख, संघर्षों, तनावों-उलझनों से जुड़ी हो वह रचना जनवादी ही होती है। उसके लिए किसी विशिष्ट नीति या ढाँचे में फिट होने की जवाबदारी नहीं है। कहानी परम्परा से हमारे पास आयी है और अरसे से बदलते सन्दर्भों से जुड़कर सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करती रही है। समय की गाथा होते हुए भी कहानी की दृष्टि आगामी कल पर होती है। कहानी का जन्म ही आपसी सुख-दुःख बाँटने की इच्छा के साथ हुआ। यही निश्चछल संवाद कहानी का मूल है। वक्त के हालात के साथ जुड़कर उसमें वक्त का दर्द भरा चेहरा उभर आया। स्थितियों के प्रभाव को झेलते आम जन का भीतरी एवं बाहरी परिवेश झलक पड़ा, जो स्वाभाविक था। क्योंकि साहित्य समय का आईना है।
अपने रचना-कर्म के दौरान मैंने पाया कि रचनाकार पहले-पहले निजी सुख-दुःख से ज़्यादा जुड़ा रहता है और धीरे-धीरे अनुभव सम्पन्नता से रचकर वृहत्तर समाज के सुख-दुख का भोक्ता बनने लगता है। मेरे लिए लेखन जहां भोगे हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति है वहीं अनुभव किये सत्य की भी।
मैंने जिन सन्दर्भ एवं स्थितियों को शिद्दत से महसूस किया, व्यवस्था के जिन दंशो ने मुझे दंशित किया है। मैंने उन्हें अपनी रचनाओ में डाला। मैंने जिस आत्मीयता एवं मार्मिकता के साथ अपने सत्यों को ‘पोशनूल की वापसी’ ‘ओ सोनकिसरी’ ‘तैंतीबाई’ आदि कहानियों और ‘ऐलान गली जिन्दा है’ ‘यहाँ वितस्ता बहती है’ आदि उपन्यासों में अभिव्यक्ति कर आम आदमी का सच बनाया, उसी आत्मीयता के एवं जीवन्तता के साथ अनुभूत यथार्थ का ‘आत्मबोध’, ‘सिद्धि का कटरा’, ‘नूरा बाई’, ‘पत्थरों के राग’ ‘अन्तिम साक्ष्य’, ‘अपने-अपने कोणार्क’ आदि कृतियों में ढालकर पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। अब अपने-पराये का फर्क करना ही बेमानी लगता है। अनुभूतियों के विविधवर्णी सागर में डुबकियां लगाते हम सभी कहीं-न कहीं एक रंग दिखाई देते हैं। शायद बहुत गहरे, कहीं हैं भी। ‘पत्थरों के राग’ कहानी पढ़कर मेरी मित्र ओड़िया लेखिका प्रतिभा राय ने कहा-‘लगता है, तूने कहानी नायिका सोनल का दर्द भोगा है, नहीं को इतनी मार्मिकता और जीवन्तता दूसरे के दुख को स्वर देते नहीं आती।’’ जबकि उसे मालूम है कि मेरी तो किशोरावस्था के प्रथम चरण में ही शादी हो गयी थी मेरा उपन्यास ‘बाक़ी सब खैरियत है’, जब टाइप हो रहा था, तो मेरे टाइपिस्ट शर्माजी बोले कि आपको हमारे घरेलू हालात कैसे मालूम पड़े ? मेंने तो कभी ज़िक्र नहीं किया...।’’
सच तो यह है कि इस उपन्यास में काफ़ी कुछ मेरे निजी परिवेश का यथार्थ जुड़ा हुआ है, जो अनायास ही दूसरों का यथार्थ बन गया। बहरहाल, कहना यही है कि जब हमारा निजी सच वृहत्तर समाज का सच बन जाता है तभी साहित्य बन जाता है।
साहित्य शब्द में ही तो सहित का भाव जुड़ा है। हमारे अपने सुख-दुःख भी सामाजिक आर्थिक परिवेश की उपज होते हैं,विविध व्यवस्थाओं के परिणाम होते हैं।
अकसर किसी बादाम, नाशपाती या अखरोट के पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ती-गिराती अधकुतरे मीठे फल फ्रॉक के घेर में इकट्ठा करती, चीड़ की कटी-टहनियां बटोरती, यह लड़की हाँफती, पसीना-पसीना हुई पहाड़ी पर बने बँगलों में दाखिल हो जाती है, जहाँ एक हाल नुमा हवादार कमरे में तीमारदारों से घिरी एक औरत पलंग पर लेटी होती है। बच्ची बड़े एहतियात से चीड़ की टहनियाँ उसके सिरहाने सजा देती है। डाक्टरों ने जो उस स्त्री को शुद्ध हवा सेवन के लिए शहर के पंचमंज़िला घर से वुरपश गाँव के इस छोटे से बँगलें में रहने के लिए सलाह दी है। अधकुतरे मीठे बादाम, अखरोट जबरदस्ती स्त्री के मुँह में भरने पर लड़की डाँट खाती है पर सिर झटककर हँस देती है। क्योंकि उसके मन में अखण्ड विश्वास है यह तपेदिक की मरीज औरत, जिसकी भूख और उम्र तेज़ी से घट रही है, जो इंच-दर-इंच मौत के करीब खिसकती जा रही है, उसके चुन-चुन कर लाए फल–फूल और चीड़ की कटी टहनियों में जीवन की संजीवनी से जी उठेगी। यह औरत, जो उसकी मां है, मौत के बिस्तर पर भी चिन्तित है कि उसकी इस ‘कलन्दर’ बेटी का क्या होगा ? क्या इसलिए कि लड़की घर के सम्भ्रान्त अनुशासनों में बँध नहीं पाती, लीक तोड़कर चलना चाहती है ?
और जब एक दिन चीड़-देवदार की शफ्फाक हवाओं की गोद में भी वह पलंग खाली हो गया तो वह छः सात वर्ष की चहचहाती बालिका सुग्गे, गुगी और पोशनूल से बतियाना भूल, उम्र से पहले ही बड़ी हो गयी। चुप गुमसुम और अपने भीतर तेजी से कुछ घटने लगा। चीज़ें अपनी शक्लें बदलने लगीं। आकाश का नीला विस्तार एक दमघोंट खोह में क़ैद हो गया। आसमान को अपने पैरों तले तौलने वाले रंगीन पाँखी उसकी नज़रों से दूर चले गये। उसके बाद वह लड़की कभी उन खुली पगडण्डियों पर नहीं दौड़ी उसके भीतर उगमती बेइन्तहा बातें, कौतुक भरे प्रश्न जमकर ग्लेशियर बनते गये। वह बहन-भाई पिता-किसी से भी अपने भीतर उगते बेसिर-पैर के प्रश्न नहीं पूछ पाई। उसने ‘ढंग से’ बात करना, कहना, सीखा ही कहाँ था। तब बारह वर्ष की उम्र में उसने पहली कविता लिखी-‘भर आता जब यह मौन हृदय....’’ क्या भीतर जो घट रहा था उसे जानने के लिए ? ज़रूर यह छुई-मुई उम्र की भावुक अभिव्यक्ति थी, पर महत्त्वपूर्ण इसलिए कि वे पहले-पहले शब्द थे जो मेरे भीतर से पहाड़ी झरने की तरह फटे थे। और उन्हें अपने घरवालों से छिप कर मैंने कागज पर उतारा था। मेरे रचनाकार के जन्म की शुरूआत वही थी। इसलिए मैं आज भी मानती हूँ रचनाकार का जन्म दुख से होता है।
घटनाएँ जीवन में बहुत घटीं, उनका प्रभाव भी मुझ पर पड़ा, पर सभी के साथ घटनाएं घटती हैं। हमारे व्यक्तित्व में कुछ भी जोड़-तोड़ करती हैं। एक घटना, जिसने बचपन को लाँघकर मुझे एकदम ढेर सारे दायित्वों के बीच खड़ा कर बड़ा बना दिया-बहुत छोटी उम्र में पिता की देहरी छोड़नी थी। हमारे विद्वान पिता, प्रोफ़ेसर रामचन्द्र पण्डित ने नारी शिक्षा के हिमायती होने के बावजूद, हम दोनों बहनों के लिए घर और वर समय से पहले ही जुटा लिए। तमाम दानिशमन्दी के बावजूद वे तेजी से बढ़ती अपनी वय से शायद आशंकित थे। उनकी आशंका अपनी जगह सही भी थी, बिना माँ की बेटियों के भविष्य के लिए मेरे लिए यह दूसरा धक्का था, क्योंकि नये घर में तमाम प्यार और आदर की हक़दार होने के बावजूद मुझे लगा कि किसी ने बढ़ी बेदर्दी से आकाश में उड़ान भरते पाँखी के पंख कतर दिये हैं और उसे सोने के पिजड़े में कैद कर दिया है, जो अब उम्र क़ैद है, साल भर इस कैद में आसूं बहाते मैं यह समझ गयी कि क़ैदें ज़िन्दगी की ज़रूरी शर्तें हैं, पर मन में एक ढीठ निश्चय ही उभरता गया कि मेरा मन आसमान की ऊँचाइयाँ छूता रहा है। मैं छोटी उम्र में ही बेहतर कल्पनाशील बन गयी। कुछ करने और बनने की जिद मुझे अक्सर बेचैन रखती। ज़रूर मेरे पति डाक्टर विशिन ने जो तब स्वयं बी.एस.सी के छात्र थे और मेरे ससुराल वालों ने, मेरी कुछ बनने और पाने की ज़िद को समझा और मेरे रास्ते में रुकावटे नहीं डालीं। इसलिए तमाम पारस्परिक मान्यताओं व संहिताओं बीच मैं घर की बड़ी बहू एक बेटी की तरह घर में रही, स्कूल कॉलेज में अपना अध्ययन-मनन ज़ारी रखा।
समय को तो बीतना ही होता है। मैं छिटपुट कविताएं स्कूल-कॉलेज की पत्रिकाओं में लिखती रही। श्रीनगर में गर्ल्स कॉलेज में, फिर गाँधी मेमोरियल कॉलेज में कुछ कविताएं-कुछ कहानियाँ छपीं। एम.ए. करते समय, बिरला कॉलेज पिलानी में एक बार हमारे प्रिंसिपल डॉ. कन्हैयालाल सहल ने कविता प्रतियोगिता के लिए मुझसे एक कविता लिखवायी, जो बाद में पुरस्कृत भी हुई। उस बार पिलानी के विरला ऑडियाटोरियम में पुरस्कार वितरण समारोह में डॉ. सहल ने निरन्तर लिखने और लेखन के उत्तरोत्तर विकास सम्बन्धी जो बातें मुझसे कहीं उनसे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। पिलानी में दो वर्ष अध्यापन करने के बाद मैं अपने पति डॉ. विशिन के साथ हैदराबाद चली गयी। वहींसे मेरा नियमित लेखन आरम्भ हुआ। मैंने नौकरी छोड़कर स्वतन्त्र लेखन का दायित्व उठा लिया। मुझसे नौकरी, लेखक और गृहस्थी साथ-साथ नहीं निभे। चुनाव मेरा अपना था। मेरे पति ने मेरे रास्ते में कभी कोई बाधा नहीं डाली।
सितम्बर 1967 में कल्पना (हैदराबाद) में मेरी पहली कहानी ‘खून के रेशे’ प्रकाशित हुई। उसी वर्ष अक्टूबर में नयी कहानियाँ’ में ‘कैक्टस’ और अगले वर्ष ‘ज्ञानोदय’ में ‘सलाखों के पीछे’’ आदि कहानियाँ प्रकाशित हुई। बाद में धीरे-धीरे अन्य व्यावसायिक-अव्यावसायिक पत्रिकाओं में बराबर लिखती रही। जिस दौर में मैंने नियमित लेखन शुरू किया कथा-जगत में वह दौर काफी बहस-मुबाहसों एवं नये प्रयोगों का दौर था।
नयी कहानी के विरोध में ‘अकहानी’ का नारा बुलन्द किया जा रहा था और कामूकाफ्का की भौंड़ी नकल के फलस्वरूप ‘सन्त्रास’ और सेक्स’ फ़ैशन बनाकर भुनाया जा रहा था। नयी कहानी वाले दौर की तरह ही अनकही के लेखक अपने पूर्ववर्ती लेखकों को अस्वीकार करने लगे थे। उन दिनों अमृतराय ‘नयी कहानियाँ’ का सम्पादन करते थे और मैं बराबर उसमें लिख रही थी। अमृत जी ने ‘‘सार्थक विद्रोह, दशा-दिशा-संभावना’ नाम से एक लेखमाला में ‘सार्थक कहानी’ पर एक बहस की शुरूआत की जिसमें छद्म आधुनिकता का विरोध किया गया और लेखन को समकालीन जीवन एवं भोगे हुए यथार्थ से जोड़कर जीवनास्था पर बल दिया गया मुझे ‘नयी कहानियाँ’ के इस स्तम्भ ने दिशा दी, यह मैं आज भी मानती हूँ।
उसके बाद कहानी सचेतन सामान्तर, जनवादी आदि खेमों में बाँटी गयी। अलग-अलग खेमों अलग-अलग अलमबदार और आलोचक बन गये। पर खेमों ने मुझे कभी आकर्षित नहीं किया। मैं बराबर लिखती रही और अपने लेखन को सँवारती रही। साहित्य पुराना, परम्परावादी या रूढ़ हो सकता है, यह बात आज भी मैं नहीं मानती। समय के इस दस्तावेज को समय के सन्दर्भों के साथ जोड़कर देखने पर भी यह बात स्पष्ट है कि साहित्यकार समय की सीमा के पार देखता और सोचता है। मानवीय संवेगों और स्थितियों से सम्बन्ध रखने के कारण युगों तक हमें अपने भीतर झांकने, सीखने और जीने की प्रेरणा देता है। वह चाहे कथा सरित्सागर, उपनिषद कथाएँ, चन्द्रकान्ता सन्तति हो या तुलसी, कबीर, कालिदास, प्रेमचन्द की रचनाएं हों। साहित्य जीवन की मूलभूत शर्तों से जुड़ा होने के कारण पुराना पड़ नहीं सकता। तभी तो हम टाल्सटाय, गोर्खी, चेखव, दास्तोएवस्की हेमिंग्वे, कालिदास आदि को आज भी बड़े चाव और उत्सुकता से पढ़ते हैं।
नयी कहानी के दौर वालों वालों ने अज्ञेय जैनेन्द्र आदि का विरोध किया तो अनकही वाले खेमे ने साठोत्तरी लेखन से नयी कहानी के रचनाकारों को खारिज कर दिया। दरअसल विरोध की यह नीति ही ग़लत थी। तुलसी, प्रेमचन्द, उग्र, जैनेन्द्र, अज्ञेय, मुक्ति, बोध, राकेश, धर्मवीर, भारती, राजेन्द्र यादव, भीष्म साहनी हमारी अगली पीढ़ियाँ गर्व करेंगी। मैं तब भी मानती थी और आज भी मानती हूँ कि साहित्यकार प्रगतिशील ही होता है। दकियानूसी, वक्त की धार से कटा हुआ कोई भी रचनाकार जीवन के विशाल फलक को खुली आँखों और खुले मन से दूर तक देख नहीं सकता। अतीत, वर्तमान और आगत के चेहरों को पढ़ कर उन्हें सँवारने का स्वप्न देख नहीं सकता। मेरे विचार में जो रचना आम जन के दुःख-सुख, संघर्षों, तनावों-उलझनों से जुड़ी हो वह रचना जनवादी ही होती है। उसके लिए किसी विशिष्ट नीति या ढाँचे में फिट होने की जवाबदारी नहीं है। कहानी परम्परा से हमारे पास आयी है और अरसे से बदलते सन्दर्भों से जुड़कर सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करती रही है। समय की गाथा होते हुए भी कहानी की दृष्टि आगामी कल पर होती है। कहानी का जन्म ही आपसी सुख-दुःख बाँटने की इच्छा के साथ हुआ। यही निश्चछल संवाद कहानी का मूल है। वक्त के हालात के साथ जुड़कर उसमें वक्त का दर्द भरा चेहरा उभर आया। स्थितियों के प्रभाव को झेलते आम जन का भीतरी एवं बाहरी परिवेश झलक पड़ा, जो स्वाभाविक था। क्योंकि साहित्य समय का आईना है।
अपने रचना-कर्म के दौरान मैंने पाया कि रचनाकार पहले-पहले निजी सुख-दुःख से ज़्यादा जुड़ा रहता है और धीरे-धीरे अनुभव सम्पन्नता से रचकर वृहत्तर समाज के सुख-दुख का भोक्ता बनने लगता है। मेरे लिए लेखन जहां भोगे हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति है वहीं अनुभव किये सत्य की भी।
मैंने जिन सन्दर्भ एवं स्थितियों को शिद्दत से महसूस किया, व्यवस्था के जिन दंशो ने मुझे दंशित किया है। मैंने उन्हें अपनी रचनाओ में डाला। मैंने जिस आत्मीयता एवं मार्मिकता के साथ अपने सत्यों को ‘पोशनूल की वापसी’ ‘ओ सोनकिसरी’ ‘तैंतीबाई’ आदि कहानियों और ‘ऐलान गली जिन्दा है’ ‘यहाँ वितस्ता बहती है’ आदि उपन्यासों में अभिव्यक्ति कर आम आदमी का सच बनाया, उसी आत्मीयता के एवं जीवन्तता के साथ अनुभूत यथार्थ का ‘आत्मबोध’, ‘सिद्धि का कटरा’, ‘नूरा बाई’, ‘पत्थरों के राग’ ‘अन्तिम साक्ष्य’, ‘अपने-अपने कोणार्क’ आदि कृतियों में ढालकर पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। अब अपने-पराये का फर्क करना ही बेमानी लगता है। अनुभूतियों के विविधवर्णी सागर में डुबकियां लगाते हम सभी कहीं-न कहीं एक रंग दिखाई देते हैं। शायद बहुत गहरे, कहीं हैं भी। ‘पत्थरों के राग’ कहानी पढ़कर मेरी मित्र ओड़िया लेखिका प्रतिभा राय ने कहा-‘लगता है, तूने कहानी नायिका सोनल का दर्द भोगा है, नहीं को इतनी मार्मिकता और जीवन्तता दूसरे के दुख को स्वर देते नहीं आती।’’ जबकि उसे मालूम है कि मेरी तो किशोरावस्था के प्रथम चरण में ही शादी हो गयी थी मेरा उपन्यास ‘बाक़ी सब खैरियत है’, जब टाइप हो रहा था, तो मेरे टाइपिस्ट शर्माजी बोले कि आपको हमारे घरेलू हालात कैसे मालूम पड़े ? मेंने तो कभी ज़िक्र नहीं किया...।’’
सच तो यह है कि इस उपन्यास में काफ़ी कुछ मेरे निजी परिवेश का यथार्थ जुड़ा हुआ है, जो अनायास ही दूसरों का यथार्थ बन गया। बहरहाल, कहना यही है कि जब हमारा निजी सच वृहत्तर समाज का सच बन जाता है तभी साहित्य बन जाता है।
साहित्य शब्द में ही तो सहित का भाव जुड़ा है। हमारे अपने सुख-दुःख भी सामाजिक आर्थिक परिवेश की उपज होते हैं,विविध व्यवस्थाओं के परिणाम होते हैं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book