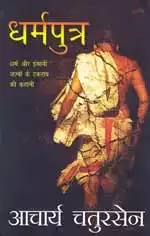|
सामाजिक >> धर्मपुत्र धर्मपुत्रआचार्य चतुरसेन
|
85 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है एक सफल उपन्यास....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
एक युवक जो कट्टर हिन्दू परिवार और परिवेश में पलता बढ़ता है और जब उसे
पता चलता है कि वह जन्म से मुसलमान है उसी के अन्तर्द्वन्द्व तथा मानसिक
संघर्ष के चारों ओर धर्मपुत्र का घटना चक्र घूमता है।
भूमिका
कृश्न चन्दर को एक पार्टी दी गई थी। पार्टी दिल्ली के एक प्रतिष्ठित
प्रकाशक ने दी थी। निमन्त्रण मुझे भी मिला। गो यह एक नई बात थी। आम तौर पर
मुझे लोग पार्टियों में बुलाते-उलाते नहीं। नई दिल्ली के एक शानदार होटल
में पार्टी का आयोजन था। पार्टी में अनेक प्रकाशक, साहित्यकार, पत्रकार और
अध्यापक भी थे। और मैं तो था ही। पार्टी की धूमधाम और शान को मैंने देखा।
कृश्न चन्दर को देखा—निपट बालक—सा तरुण है। मैं सोच
रहा
था—इसे भला क्यों पार्टी दी गई ? ऐसी शानदार पार्टी तो मुझे
मिलनी
चाहिए थी। इसके बाद अकस्मात मेरे मन में एक विचार पैदा हुआ कि क्या कारण
है अब तक मुझे किसी ने ऐसी शानदार पार्टी नहीं दी। चालीस साल कलम घिसी,
पैंसठ के देहलीज़ पर पहुंचा, ग्रंथों की संख्या एक सौ इक्कीस को पार कर
गई, फिर क्या लोग अन्धे हैं, बहरे हैं, मूर्ख हैं या साहित्य को समझते
नहीं हैं ? क्या बात है ? वास्तव में पार्टी यदि किसी और को मिलनी चाहिए
थी, तो मुझी को मिलनी चाहिए थी। मैंने एक बार आंख और सिर उठाकर चारों ओर
देखा, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उस जमघट में मुझसे बड़ा साहित्यकार तो
कोई नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी पार्टी मुझे नहीं, कृश्न चन्दर को ही दी
गई थी। इसमें तनिक भी शुबहा न था।
बड़ी देर तक मैं इस बात पर विचार करता रहा। और अन्त में मेरे मन ने मान लिया कि मैं सिर्फ आयु में ही कृश्न चन्दर से बड़ा हूं, परन्तु साहित्कार कृश्न चन्दर ही है, गो बालक ही। अब मुझे इस बात का भी पछतावा हो रहा था कि मैं तो कृश्न चंदर के सम्बन्ध में कुछ जानता ही नहीं हूं। खुदा की मार मुझ पर कि मैंने उनकी कोई कहानी पढ़ी ही नहीं। निन्दा और स्तुति मैं साहित्यकारों की सुनने का आदी नहीं। अब मैं घबराने भी लगा था कि थोड़ी देर में भाषण होंगे—कृश्न चन्दर की और उनके साहित्य की प्रशंसात्मक आलोचना करनी होगी। संभवतः यह काम मुझे ही सबसे प्रथम अंजाम देना होगा, क्योंकि यहां सबसे बड़ा साहित्यकार तो मैं ही हूं; गो कृश्न चंदर से छोटा ही सही। मगर कहाँ ? प्रशस्तिगान आरम्भ कराया गया देवेन्द्र सत्यार्थी से। मानता हूं कि उनकी जैसी शानदार दाढ़ी दिल्ली-भर में नहीं मिल सकती, हालांकि इस वक्त दिल्ली दाढ़ियों का सबसे बड़ा मार्केट है। मगर मजलिस में मैं तो था ही; उग्र थे, जैनेन्द्र और भी अनेक थे। इन सबके सिर पर लम्बी दाढ़ी की यह था नेदारी मुझे बहुत नागवार प्रतीत हुई। गो दाढ़ी-बहुत ही शानदार थी, और कला की दृष्टि से वह भी साहित्य के अन्तर्गत आती है। निरालापन ही तो साहित्य की जान है—और यह दाढ़ी जरूर निराली थी। फिर भी हम लोग के रहते हुए सिर्फ दाढ़ी ही के जोर पर उसे साहित्यिक मजलिस की नाक का बाल बनाना अप्रैल की सिर्फ पहली तारीख को ही बर्दाश्त किया जा सकता है। उग्र भी शायद गुनगुने हो रहे थे—मैं सोच ही रहा था कि दाढ़ी के बाद अब मेरी बारी आएगी। परंतु कहां ? उग्र एकदम उठ खड़े हुए। अपना परिचय दिया, जो कहना-सुनना था, कह गए।
परन्तु मेरी बारी तो फिर भी नहीं आई। बारी जैनेन्द्र की। धत्तेरे की ! अब मुझे स्वीकार करना पड़ा कि जैनेन्द्र भी मुझसे बड़े साहित्यकार हैं—यद्यपि उम्र में वे भी छोटे हैं। जैनेन्द्र का भाषण आरम्भ हुआ—और मैंने कुछ सोचना आरम्भ कर दिया। पुरानी आदत है; जैनेन्द्र जब बोलने लगते हैं तो मैं किसी विषय का चिन्तन करने लगता हूं। ध्यान से सुनने-समझने पर भी कुछ पता ही नहीं लगता कि वे क्या कह रहे हैं। बस, यही सोचकर सन्तोष कर लेता हूं कि कुछ दार्शनिक बातें कह रहे होंगे—जिससे मैं प्याज की बू तरह घबराता हूं। इसलिए, जैनेन्द्र के भाषण के साथ ही मैं अपने किसी प्रिय को सोचने लगता हूं। परन्तु उस समय जैनेन्द्र ही की बात सोचने लगा। ज़रूर ही जैनेन्द्र मुझसे बड़े साहित्यकार हैं, तभी तो सब लोग मेरे रहते भी उन्हें आगे रखते हैं—जिसमें उन्हें भी कभी संकोच नहीं हुआ। अवश्य ही वे भी ऐसा ही समझते हैं। सोचते-सोचते मन ने कहा—प्रत्येक साहित्यकार का पृथक-पृथक् ब्रांड है। जैनेन्द्र जलेबी ब्रांड साहित्यकार हैं।
उनके साहित्य में जलेबी जैसा कुछ चिपचिप चिपकता, कुछ टपकता, कुछ गोल-गोल उलझा, कुछ सुलझा—मीठा-मीठा साहित्य-रस रहता है। बासी होने पर प्रसाद कहकर बेचा जाता है। फिर मेरा ध्यान सामने बैठे उग्र पर पड़ा। निस्संदेह उग्र डंडा ब्रांड साहित्यकार हैं—सीधी खोपड़ी पर खींच मारते हैं। फिर वह बिलबिलाया करे, अस्पताल जाए या चूना-गुड़ का लेप करे। और मैं हूं लाठी ब्रांड साहित्यकार—चोट करूंगा को ठौर करके धर देना ही मेरा लक्ष्य है, सांसें आने का काम नहीं। सामने नजर उठी तो बनारसीदास चतुर्वेदी रस-गुल्लों पर हाथ साफ कर रहे थे। भई वाह, ये हैं बल्ली ब्रांड साहित्यकार। जिसका जी चाहे नापकर देख ले। लीजिए साहेब, मैं तो सोचता ही रहा और लोग उठ-उठकर घर चलने भी लगे। हड़बड़ाकर देखा—पार्टी खत्म हो चुकी थी। भाषण और भी हुए थे। कृश्न चन्दर ने जवाब में भी कुछ कहा-सुनी की थी। पर मेरी हिमाकत देखिए—मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। अब मैं समझ गया कि क्यों लोग मुझे बुलाते-उलाते नहीं। परन्तु अब क्या हो सकता था ? पछताता-पछताता घर चला आया।
बहुत गुस्सा आ रहा था सब लोगों पर। क्यों नहीं लोग मुझे ऐसी पार्टियां देते ? परन्तु कहूं किससे ? मन ही मन खीझ रहा था कि मन ने एक धक्का दिया, कहा—अपनी इतनी पूजा करता है तो दुनिया से क्या ? तू खुद अपनी ओर देख, अपना साहित्य रचे जा, अपनी कलम चलाए जा, अपने आंसू बिखेरे जा। अपनी रचना आप ही पढ़। अपनी सम्पदा से आप ही सम्पन्न रह। मगन रह। पार्टी-वार्टी को गोली मार, और उठा अपना कलम। अभी उठा। इस वक्त दिल चुटीला है—ऐसी ही चोट खाकर साहित्यिक वेदनाएं मूर्त होती हैं। खींच तो एक ‘दर्द की तस्वीर’।
क्या कहा जाए, अपने ही मन की बात, टाली नहीं जा सकी। लो साहेब, हद हो गई। हाथ आप ही कलम पर आ पड़ा। कलम था फाउंटेन पेन। इसी साल मेरे चौंसठवें जन्म-नक्षत्र पर दिल्ली की प्रगतिशील साहित्य-परिषद् ने मुझे स्नेह-भेंट के रूप में दिया था। इस सम्बन्ध में भी कुछ कहना पड़ा। आज तक किसी भी साहित्यकार, साहित्य-संस्था या साहित्य संघ ने कभी मेरे पास आकर नहीं कहा—कि आ, तुझे हम सम्मानित करें। तेरा जन्म-नक्षत्र मनाएं, तेरी कुछ धूम-धाम करें, पब्लिसिटी करें। न कभी किसी सम्मेलन का सभापति ही मुझे बनाया गया।
जारी बहुत की। सभापति बनाना तो दूर—साहित्य सम्मेलन के अधिवेशवन में कभी मुझे निमन्त्रण तक नहीं मिला। पिछली बार मेरठ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन था। वहां मैं बिना बुलाए ही चला गया—इसलिए कि पास तो है ही, बहुत-से साहित्य-बन्धुओं के दर्श-पर्श हो जाएंगे। देखा सबने, पर किसी ने भीतर मंच पर चलकर बैठने तक को नहीं कहा। दो दिन बाहर ही बाहर घूमकर चला आया। सो ऐसी हालत में हर साल मैं ही अपना जन्म-नक्षत्र मना लिया करता हूं। बन्धु-बांधव, मित्र और कुछ साहित्य-परिजन आ जाते हैं—मेरे घर को जुठार जाते हैं, मेरे प्राणों को आनन्द दे जाते हैं। पर भेंट-उपहार कभी कोई नहीं देता। इस बार न जाने यह क्या एक बदपरहेजी ही हो गई कि प्रगतिशील मंडल ने हरिदत्त भाई के हाथ मुझे एक कलम भेंट दी। उस समय मैंने यह स्वीकारोक्ति की थी कि इस कलम से पहली बार एक उपन्यास लिखूंगा। और यह भी लिख दूंगा कि—कि यह उपन्यास इस कलम से लिखा हुआ है। सो हाथ इस कलम पर आ पड़ा और वह स्वीकारोक्ति भी याद पड़ गई। बस, एक पन्थ दो काज। उसी कलम से ‘दर्द की यह तस्वीर’ खींची गई है। इस तस्वीर में दर्द जितना है वह मेरे कलेजे का है, और प्यार जितना है वह प्रगतिशील साहित्य-मंडल के सदस्यों का—जो उन्होंने अपने कलम से भरकर मेरे जन्म-नक्षत्र पर भेजा था।
बड़ी देर तक मैं इस बात पर विचार करता रहा। और अन्त में मेरे मन ने मान लिया कि मैं सिर्फ आयु में ही कृश्न चन्दर से बड़ा हूं, परन्तु साहित्कार कृश्न चन्दर ही है, गो बालक ही। अब मुझे इस बात का भी पछतावा हो रहा था कि मैं तो कृश्न चंदर के सम्बन्ध में कुछ जानता ही नहीं हूं। खुदा की मार मुझ पर कि मैंने उनकी कोई कहानी पढ़ी ही नहीं। निन्दा और स्तुति मैं साहित्यकारों की सुनने का आदी नहीं। अब मैं घबराने भी लगा था कि थोड़ी देर में भाषण होंगे—कृश्न चन्दर की और उनके साहित्य की प्रशंसात्मक आलोचना करनी होगी। संभवतः यह काम मुझे ही सबसे प्रथम अंजाम देना होगा, क्योंकि यहां सबसे बड़ा साहित्यकार तो मैं ही हूं; गो कृश्न चंदर से छोटा ही सही। मगर कहाँ ? प्रशस्तिगान आरम्भ कराया गया देवेन्द्र सत्यार्थी से। मानता हूं कि उनकी जैसी शानदार दाढ़ी दिल्ली-भर में नहीं मिल सकती, हालांकि इस वक्त दिल्ली दाढ़ियों का सबसे बड़ा मार्केट है। मगर मजलिस में मैं तो था ही; उग्र थे, जैनेन्द्र और भी अनेक थे। इन सबके सिर पर लम्बी दाढ़ी की यह था नेदारी मुझे बहुत नागवार प्रतीत हुई। गो दाढ़ी-बहुत ही शानदार थी, और कला की दृष्टि से वह भी साहित्य के अन्तर्गत आती है। निरालापन ही तो साहित्य की जान है—और यह दाढ़ी जरूर निराली थी। फिर भी हम लोग के रहते हुए सिर्फ दाढ़ी ही के जोर पर उसे साहित्यिक मजलिस की नाक का बाल बनाना अप्रैल की सिर्फ पहली तारीख को ही बर्दाश्त किया जा सकता है। उग्र भी शायद गुनगुने हो रहे थे—मैं सोच ही रहा था कि दाढ़ी के बाद अब मेरी बारी आएगी। परंतु कहां ? उग्र एकदम उठ खड़े हुए। अपना परिचय दिया, जो कहना-सुनना था, कह गए।
परन्तु मेरी बारी तो फिर भी नहीं आई। बारी जैनेन्द्र की। धत्तेरे की ! अब मुझे स्वीकार करना पड़ा कि जैनेन्द्र भी मुझसे बड़े साहित्यकार हैं—यद्यपि उम्र में वे भी छोटे हैं। जैनेन्द्र का भाषण आरम्भ हुआ—और मैंने कुछ सोचना आरम्भ कर दिया। पुरानी आदत है; जैनेन्द्र जब बोलने लगते हैं तो मैं किसी विषय का चिन्तन करने लगता हूं। ध्यान से सुनने-समझने पर भी कुछ पता ही नहीं लगता कि वे क्या कह रहे हैं। बस, यही सोचकर सन्तोष कर लेता हूं कि कुछ दार्शनिक बातें कह रहे होंगे—जिससे मैं प्याज की बू तरह घबराता हूं। इसलिए, जैनेन्द्र के भाषण के साथ ही मैं अपने किसी प्रिय को सोचने लगता हूं। परन्तु उस समय जैनेन्द्र ही की बात सोचने लगा। ज़रूर ही जैनेन्द्र मुझसे बड़े साहित्यकार हैं, तभी तो सब लोग मेरे रहते भी उन्हें आगे रखते हैं—जिसमें उन्हें भी कभी संकोच नहीं हुआ। अवश्य ही वे भी ऐसा ही समझते हैं। सोचते-सोचते मन ने कहा—प्रत्येक साहित्यकार का पृथक-पृथक् ब्रांड है। जैनेन्द्र जलेबी ब्रांड साहित्यकार हैं।
उनके साहित्य में जलेबी जैसा कुछ चिपचिप चिपकता, कुछ टपकता, कुछ गोल-गोल उलझा, कुछ सुलझा—मीठा-मीठा साहित्य-रस रहता है। बासी होने पर प्रसाद कहकर बेचा जाता है। फिर मेरा ध्यान सामने बैठे उग्र पर पड़ा। निस्संदेह उग्र डंडा ब्रांड साहित्यकार हैं—सीधी खोपड़ी पर खींच मारते हैं। फिर वह बिलबिलाया करे, अस्पताल जाए या चूना-गुड़ का लेप करे। और मैं हूं लाठी ब्रांड साहित्यकार—चोट करूंगा को ठौर करके धर देना ही मेरा लक्ष्य है, सांसें आने का काम नहीं। सामने नजर उठी तो बनारसीदास चतुर्वेदी रस-गुल्लों पर हाथ साफ कर रहे थे। भई वाह, ये हैं बल्ली ब्रांड साहित्यकार। जिसका जी चाहे नापकर देख ले। लीजिए साहेब, मैं तो सोचता ही रहा और लोग उठ-उठकर घर चलने भी लगे। हड़बड़ाकर देखा—पार्टी खत्म हो चुकी थी। भाषण और भी हुए थे। कृश्न चन्दर ने जवाब में भी कुछ कहा-सुनी की थी। पर मेरी हिमाकत देखिए—मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। अब मैं समझ गया कि क्यों लोग मुझे बुलाते-उलाते नहीं। परन्तु अब क्या हो सकता था ? पछताता-पछताता घर चला आया।
बहुत गुस्सा आ रहा था सब लोगों पर। क्यों नहीं लोग मुझे ऐसी पार्टियां देते ? परन्तु कहूं किससे ? मन ही मन खीझ रहा था कि मन ने एक धक्का दिया, कहा—अपनी इतनी पूजा करता है तो दुनिया से क्या ? तू खुद अपनी ओर देख, अपना साहित्य रचे जा, अपनी कलम चलाए जा, अपने आंसू बिखेरे जा। अपनी रचना आप ही पढ़। अपनी सम्पदा से आप ही सम्पन्न रह। मगन रह। पार्टी-वार्टी को गोली मार, और उठा अपना कलम। अभी उठा। इस वक्त दिल चुटीला है—ऐसी ही चोट खाकर साहित्यिक वेदनाएं मूर्त होती हैं। खींच तो एक ‘दर्द की तस्वीर’।
क्या कहा जाए, अपने ही मन की बात, टाली नहीं जा सकी। लो साहेब, हद हो गई। हाथ आप ही कलम पर आ पड़ा। कलम था फाउंटेन पेन। इसी साल मेरे चौंसठवें जन्म-नक्षत्र पर दिल्ली की प्रगतिशील साहित्य-परिषद् ने मुझे स्नेह-भेंट के रूप में दिया था। इस सम्बन्ध में भी कुछ कहना पड़ा। आज तक किसी भी साहित्यकार, साहित्य-संस्था या साहित्य संघ ने कभी मेरे पास आकर नहीं कहा—कि आ, तुझे हम सम्मानित करें। तेरा जन्म-नक्षत्र मनाएं, तेरी कुछ धूम-धाम करें, पब्लिसिटी करें। न कभी किसी सम्मेलन का सभापति ही मुझे बनाया गया।
जारी बहुत की। सभापति बनाना तो दूर—साहित्य सम्मेलन के अधिवेशवन में कभी मुझे निमन्त्रण तक नहीं मिला। पिछली बार मेरठ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन था। वहां मैं बिना बुलाए ही चला गया—इसलिए कि पास तो है ही, बहुत-से साहित्य-बन्धुओं के दर्श-पर्श हो जाएंगे। देखा सबने, पर किसी ने भीतर मंच पर चलकर बैठने तक को नहीं कहा। दो दिन बाहर ही बाहर घूमकर चला आया। सो ऐसी हालत में हर साल मैं ही अपना जन्म-नक्षत्र मना लिया करता हूं। बन्धु-बांधव, मित्र और कुछ साहित्य-परिजन आ जाते हैं—मेरे घर को जुठार जाते हैं, मेरे प्राणों को आनन्द दे जाते हैं। पर भेंट-उपहार कभी कोई नहीं देता। इस बार न जाने यह क्या एक बदपरहेजी ही हो गई कि प्रगतिशील मंडल ने हरिदत्त भाई के हाथ मुझे एक कलम भेंट दी। उस समय मैंने यह स्वीकारोक्ति की थी कि इस कलम से पहली बार एक उपन्यास लिखूंगा। और यह भी लिख दूंगा कि—कि यह उपन्यास इस कलम से लिखा हुआ है। सो हाथ इस कलम पर आ पड़ा और वह स्वीकारोक्ति भी याद पड़ गई। बस, एक पन्थ दो काज। उसी कलम से ‘दर्द की यह तस्वीर’ खींची गई है। इस तस्वीर में दर्द जितना है वह मेरे कलेजे का है, और प्यार जितना है वह प्रगतिशील साहित्य-मंडल के सदस्यों का—जो उन्होंने अपने कलम से भरकर मेरे जन्म-नक्षत्र पर भेजा था।
-चतुरसेन
26 अगस्त, 1954
धर्मपुत्र
मई के अन्तिम दिन। दिल्ली जैसे भाड़ में भूनी जा रही थी। पंखा आग के
थपेड़े मार रहा था। डाक्टर अमृतराय ने अपने अन्तिम रोगी को बेबाक किया और
कुर्सी छोड़ी। परन्तु उसी समय एक कार डिस्पेंन्सरी के सामने आकर रुकी।
डाक्टर ने घड़ी की ओर नज़र घुमाई, एक बज रहा था। उसकी भृकुटी में बल पड़
गए—भुनभुनाकर उसने कहा, ‘‘नहीं, इस समय अब
कोई मरीज़
नहीं देखा जाएगा।’ परन्तु उसने देखा—एक भद्र बूढ़ा
मुसलमान
कार से उतर हाथ की कीमती छड़ी के सहारे धीरे-धीरे डिस्पेन्सरी की सीढ़ियों
पर चढ़ रहा है।
कार निहायत कीमती और नई थी। वृद्ध की आयु अस्सी के ऊपर होगी। लम्बा, छरहरा और कभी का सुन्दर कमनीय शरीर सूखकर झुर्रियों से भर गया था। कमर झुक गई थी। और अब जैसे वृद्ध की दोनों टांगे उसके शरीर के भार को उठाने मे असमर्थ हो रही थीं, इसीसे वह एक कीमती नाजुक मलक्का छड़ी के सहारे आगे बढ़ रहा था। बदन पर महीन तनजेब का चिकनदार कुर्ता, और उस अतलस की अद्धी। सिर पर डेढ़ माशे की लखनउवा दुपल्ली टोपी, पुराने फैशन के कटे बाल ! ढीला पायजामा और वसली के सलीमशाही जूते। वृद्ध का उज्जवल गौर वर्ण उसकी बगुले के पर जैसी सफेद दाढ़ी-मूंछों से स्पर्द्धा-सा कर रही था। बड़ी-बड़ी आंखों में लाल डोरे उसके अतीत रुआबदार जीवन की साक्षी दे रहे थे। उन्नत ललाट और उभरी हुई नाक तथा पतले सम्पुटित होंठ उसके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना रहे थे।
वृद्ध ने भीतर आकर मुस्लिम तरीके से दोनों हाथ बढ़ाकर डाक्टर के हाथ अपने हाथों में लेकर अभिवादन किया। फिर कुछ कांपती-सी धीमी आवाज़ में कहा, ‘‘मुआफ कीजिए, मैंने बेवक्त आपको तकलीफ दी। ओफ, किस शिद्दत की गर्मी है, आग बरस रही है। यह आपके आराम करने का वक्त है, लेकिन मैं भीड़ से बचने और तख्लिये में आपसे मिलने की खातिर ही देर से आया।’ इतना कहकर जेब से पर्स निकाला और बत्तीस रुपयों के नोट टेबल पर आहिस्ता से रखकर वह डाक्टर के मुंह की ओर देखने लगा।
नकद फीस को देख तथा वृद्ध के अस्तित्व से प्रभावित होकर डाक्टर ने नम्रता पूर्वक कहा, ‘कोई बात नहीं। मुझे तो रोज ही इस वक्त तक बैठना पड़ता है। फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं ! लेकिन आप कृपाकर बैठिए तो।’
‘अब इस वक्त नहीं, फिर कभी, जब आपको फुर्सत हो। जब कि हम लोग इत्मीनान से बातें कर सकें।’
‘तो कल, इसी वक्त।’
‘बेहतर, लेकिन इन गर्मी में तो मेरी जान ही निकल जाएगी।’ बूढ़ा भुनभुनाया। और उसी तरह डाक्टर के हाथों को अपने हाथ में लेकर उन्हें आंखों से लगाया और कहा, ‘खुदा हाफिज़।’
वह चल दिया। डाक्टर ने बाहर आकर उसे सादर विदा किया। कार के जाने के बाद डाक्टर बड़ी देर तक उसी की बात सोचता रहा—अवश्य ही यह बूढ़ा सनकी रईस किसी रहस्य से सम्बन्धित है।
कार निहायत कीमती और नई थी। वृद्ध की आयु अस्सी के ऊपर होगी। लम्बा, छरहरा और कभी का सुन्दर कमनीय शरीर सूखकर झुर्रियों से भर गया था। कमर झुक गई थी। और अब जैसे वृद्ध की दोनों टांगे उसके शरीर के भार को उठाने मे असमर्थ हो रही थीं, इसीसे वह एक कीमती नाजुक मलक्का छड़ी के सहारे आगे बढ़ रहा था। बदन पर महीन तनजेब का चिकनदार कुर्ता, और उस अतलस की अद्धी। सिर पर डेढ़ माशे की लखनउवा दुपल्ली टोपी, पुराने फैशन के कटे बाल ! ढीला पायजामा और वसली के सलीमशाही जूते। वृद्ध का उज्जवल गौर वर्ण उसकी बगुले के पर जैसी सफेद दाढ़ी-मूंछों से स्पर्द्धा-सा कर रही था। बड़ी-बड़ी आंखों में लाल डोरे उसके अतीत रुआबदार जीवन की साक्षी दे रहे थे। उन्नत ललाट और उभरी हुई नाक तथा पतले सम्पुटित होंठ उसके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना रहे थे।
वृद्ध ने भीतर आकर मुस्लिम तरीके से दोनों हाथ बढ़ाकर डाक्टर के हाथ अपने हाथों में लेकर अभिवादन किया। फिर कुछ कांपती-सी धीमी आवाज़ में कहा, ‘‘मुआफ कीजिए, मैंने बेवक्त आपको तकलीफ दी। ओफ, किस शिद्दत की गर्मी है, आग बरस रही है। यह आपके आराम करने का वक्त है, लेकिन मैं भीड़ से बचने और तख्लिये में आपसे मिलने की खातिर ही देर से आया।’ इतना कहकर जेब से पर्स निकाला और बत्तीस रुपयों के नोट टेबल पर आहिस्ता से रखकर वह डाक्टर के मुंह की ओर देखने लगा।
नकद फीस को देख तथा वृद्ध के अस्तित्व से प्रभावित होकर डाक्टर ने नम्रता पूर्वक कहा, ‘कोई बात नहीं। मुझे तो रोज ही इस वक्त तक बैठना पड़ता है। फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं ! लेकिन आप कृपाकर बैठिए तो।’
‘अब इस वक्त नहीं, फिर कभी, जब आपको फुर्सत हो। जब कि हम लोग इत्मीनान से बातें कर सकें।’
‘तो कल, इसी वक्त।’
‘बेहतर, लेकिन इन गर्मी में तो मेरी जान ही निकल जाएगी।’ बूढ़ा भुनभुनाया। और उसी तरह डाक्टर के हाथों को अपने हाथ में लेकर उन्हें आंखों से लगाया और कहा, ‘खुदा हाफिज़।’
वह चल दिया। डाक्टर ने बाहर आकर उसे सादर विदा किया। कार के जाने के बाद डाक्टर बड़ी देर तक उसी की बात सोचता रहा—अवश्य ही यह बूढ़ा सनकी रईस किसी रहस्य से सम्बन्धित है।
2
दूसरे दिन ठीक समय पर बूढ़ा आ पहुँचा। इस समय कार की खिड़कियों में दुहरे
शीशे जड़े थे और भीतर गहरे आस्मानी साटन के पर्दे लगे थे। डाक्टर बूढ़े के
अभिप्राय को कुछ-कुछ समझ गया और उसने पहले से ही यहां एकान्त की सब सम्भव
व्यवस्था कर रखी थी।
डिस्पेन्सरी में आकर बूढ़े ने उसी भांति मुस्लिम पद्धति से डाक्टर का अभिवादन किया; एक बार डिस्पेन्सरी पर सतर्क दृष्टि डाली और बत्तीस रुपये मेज पर रखकर कहा, ‘‘क्या यहां हम इत्मीनान से बातें कर सकते हैं ?’
‘यकीनन,’ डाक्टर ने जवाब दिया।
तो मैं बताऊँ ! उसने साभिप्राय दृष्टि से डाक्टर की ओर देखा।
डाक्टर की आंखें कार की नीले साटन से ढकी हुई खिड़कियों की ओर उठ गईं। उसने आहिस्ता से कहा, ‘जैसा आप मुनासिब समझें।’
बूढ़ा उसी भाँति छड़ी टेकता हुआ कार तक गया। कार का दरवाज़ा खुला और कीमती काली सिल्क का बुर्का ओढ़े हुए एक किशोरी ने हाथ बढ़ाकर अपने चम्पे की कली के समान कोमल उंगलियों से बूढ़े का हाथ पकड़ लिया। हाथ का सहारा लेकर वह नीचे उतरी और धीरे-धीरे लाल मखमल के जूतों से सुशोभित उसके चरण आगे बढ़कर डिस्पेन्सरी की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे।
बाला का सर्वांग बुर्के से ढका था। केवल उन मखमली जूतों के बाहर उसके उज्ज्वल चरणों का जो भाग खुला दीख पड़ता था—तथा चम्पे की कली के समान जो दो उँगलियां बुर्के से बाहर बूढ़े के हाथ को पकड़े थीं—उसी से उस अनिन्द्य सुन्दरी की सुषमा का डाक्टर ने अनुमान कर लिया। वह भीता-चकिता हरिणी के समान रुकती-अटकती सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसका सीधा-लम्बा और दुबला-पतला शरीर और बहुत संकोच-सावधानी से छिपाया हुआ प्रच्छन्न यौवन डाक्टर को विचलित कर गया। उसकी बोली बन्द हो गई। उसके मुंह से बात ही नहीं निकली।
सबसे यथास्थान बैठ जाने पर वृद्ध ने एक बार छिपी नज़रों से बाला की ओर, फिर डाक्टर की ओर देखा तब कहा :
‘शायद आपने मेरा नाम सुना हो, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है।’
‘आप रंगमहल वाले नवाब मुश्ताक अहमद सालार जंग बहादुर हैं ?’’ डाक्टर ने कुछ झिझकते हुए और आदर प्रदर्शित करते हुए कहा।
‘जी हां, और आपके वालिद मरहूम-खुदा उन्हें जन्नत दे—मेरे गहरे दोस्त थे। मेरी ही सलाह से उन्होंने आपको विलायत पढ़ने को भेजा था।’
‘मैं अच्छी तरह हुजूर के नाम से वाकिफ हूं। पिताजी ने मुझसे अक्सर आपका जिक्र किया है, और यह भी बताया था कि आप ही ने मेरी विलायत की तालीम का कुल सर्फा उठाया था। वे मरते दम तक आपका नाम रटते रहे, लेकिन मुलाकात न हो सकी। आप शायद यहां अरसे से नहीं रहते हैं ?’
‘जी हां, मैं अरसे से कराची में रह रहा हूं। कल ही हम लोग मसूरी से आए हैं। इधर कई साल से मैं गर्मी में मसूरी ही रहता हूं।’
‘आपने दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब फरमाइए, आपकी क्या सेवा मैं कर सकता हूं ?’
‘शुक्रिया !’ नवाब ने अजब अन्दाज से सिर झुकाया, आंखें बन्द कीं और क्षण-भर कुछ सोचा, फिर जैसे एकाएक साहस मन में लाकर कहा, ‘यह मेरी पोती शहजादी हुस्नबानू है। मां-बाप इसके कोई नहीं हैं। मेरी भी अब कोई दूसरी औलाद नहीं है। यही वारिस है। बात, इसी के मुतल्लिक होगी।’
‘मर्ज़ क्या है ?’ डाक्टर ने सहज स्वभाव से पूछा।
‘मर्ज़ ? मर्ज़ बेआबरुई।’
डाक्टर कुछ भी समझ न सका। उसने अचकचाकर बाला की ओर देखा जो इस समय बुर्के के भीतर पीपल के पत्ते के समान कांप रही थी, फिर उसने प्रश्नसूचक दृष्टि नवाब के चेहरे पर अटक गई।
बूढ़े ने अब अकंपित वाणी से कहा, ‘शायद इस नये मर्ज़ का नाम आपने अभी न सुना हो। आप बड़े डाक्टर तो ज़रूर हैं, पर नये हैं, नौजवान हैं। ज़िन्दगी सलामत रही तो आप देखेंगे कि ऐसी बीमारियां आम होती हैं, खासकर बड़े घरों में तो बेहद तकलीफ देह हो जाती हैं।’ एक दार्शनिक-सा भाव उसकी आंखों और होंठों में खेल गया। डाक्टर उलझन में पड़ गया। उसने कहा, ‘मिहरबानी करके ज़रा साफ-साफ कहिए, मामला क्या है ?’
‘यही मुनासिब भी है। लड़की हामिला है। उम्र बाईस साल की है। और इसी नवंबर में इसकी शादी वज़ीर अलीखां से होना करार पा चुका है।’
डिस्पेन्सरी में आकर बूढ़े ने उसी भांति मुस्लिम पद्धति से डाक्टर का अभिवादन किया; एक बार डिस्पेन्सरी पर सतर्क दृष्टि डाली और बत्तीस रुपये मेज पर रखकर कहा, ‘‘क्या यहां हम इत्मीनान से बातें कर सकते हैं ?’
‘यकीनन,’ डाक्टर ने जवाब दिया।
तो मैं बताऊँ ! उसने साभिप्राय दृष्टि से डाक्टर की ओर देखा।
डाक्टर की आंखें कार की नीले साटन से ढकी हुई खिड़कियों की ओर उठ गईं। उसने आहिस्ता से कहा, ‘जैसा आप मुनासिब समझें।’
बूढ़ा उसी भाँति छड़ी टेकता हुआ कार तक गया। कार का दरवाज़ा खुला और कीमती काली सिल्क का बुर्का ओढ़े हुए एक किशोरी ने हाथ बढ़ाकर अपने चम्पे की कली के समान कोमल उंगलियों से बूढ़े का हाथ पकड़ लिया। हाथ का सहारा लेकर वह नीचे उतरी और धीरे-धीरे लाल मखमल के जूतों से सुशोभित उसके चरण आगे बढ़कर डिस्पेन्सरी की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे।
बाला का सर्वांग बुर्के से ढका था। केवल उन मखमली जूतों के बाहर उसके उज्ज्वल चरणों का जो भाग खुला दीख पड़ता था—तथा चम्पे की कली के समान जो दो उँगलियां बुर्के से बाहर बूढ़े के हाथ को पकड़े थीं—उसी से उस अनिन्द्य सुन्दरी की सुषमा का डाक्टर ने अनुमान कर लिया। वह भीता-चकिता हरिणी के समान रुकती-अटकती सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसका सीधा-लम्बा और दुबला-पतला शरीर और बहुत संकोच-सावधानी से छिपाया हुआ प्रच्छन्न यौवन डाक्टर को विचलित कर गया। उसकी बोली बन्द हो गई। उसके मुंह से बात ही नहीं निकली।
सबसे यथास्थान बैठ जाने पर वृद्ध ने एक बार छिपी नज़रों से बाला की ओर, फिर डाक्टर की ओर देखा तब कहा :
‘शायद आपने मेरा नाम सुना हो, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है।’
‘आप रंगमहल वाले नवाब मुश्ताक अहमद सालार जंग बहादुर हैं ?’’ डाक्टर ने कुछ झिझकते हुए और आदर प्रदर्शित करते हुए कहा।
‘जी हां, और आपके वालिद मरहूम-खुदा उन्हें जन्नत दे—मेरे गहरे दोस्त थे। मेरी ही सलाह से उन्होंने आपको विलायत पढ़ने को भेजा था।’
‘मैं अच्छी तरह हुजूर के नाम से वाकिफ हूं। पिताजी ने मुझसे अक्सर आपका जिक्र किया है, और यह भी बताया था कि आप ही ने मेरी विलायत की तालीम का कुल सर्फा उठाया था। वे मरते दम तक आपका नाम रटते रहे, लेकिन मुलाकात न हो सकी। आप शायद यहां अरसे से नहीं रहते हैं ?’
‘जी हां, मैं अरसे से कराची में रह रहा हूं। कल ही हम लोग मसूरी से आए हैं। इधर कई साल से मैं गर्मी में मसूरी ही रहता हूं।’
‘आपने दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब फरमाइए, आपकी क्या सेवा मैं कर सकता हूं ?’
‘शुक्रिया !’ नवाब ने अजब अन्दाज से सिर झुकाया, आंखें बन्द कीं और क्षण-भर कुछ सोचा, फिर जैसे एकाएक साहस मन में लाकर कहा, ‘यह मेरी पोती शहजादी हुस्नबानू है। मां-बाप इसके कोई नहीं हैं। मेरी भी अब कोई दूसरी औलाद नहीं है। यही वारिस है। बात, इसी के मुतल्लिक होगी।’
‘मर्ज़ क्या है ?’ डाक्टर ने सहज स्वभाव से पूछा।
‘मर्ज़ ? मर्ज़ बेआबरुई।’
डाक्टर कुछ भी समझ न सका। उसने अचकचाकर बाला की ओर देखा जो इस समय बुर्के के भीतर पीपल के पत्ते के समान कांप रही थी, फिर उसने प्रश्नसूचक दृष्टि नवाब के चेहरे पर अटक गई।
बूढ़े ने अब अकंपित वाणी से कहा, ‘शायद इस नये मर्ज़ का नाम आपने अभी न सुना हो। आप बड़े डाक्टर तो ज़रूर हैं, पर नये हैं, नौजवान हैं। ज़िन्दगी सलामत रही तो आप देखेंगे कि ऐसी बीमारियां आम होती हैं, खासकर बड़े घरों में तो बेहद तकलीफ देह हो जाती हैं।’ एक दार्शनिक-सा भाव उसकी आंखों और होंठों में खेल गया। डाक्टर उलझन में पड़ गया। उसने कहा, ‘मिहरबानी करके ज़रा साफ-साफ कहिए, मामला क्या है ?’
‘यही मुनासिब भी है। लड़की हामिला है। उम्र बाईस साल की है। और इसी नवंबर में इसकी शादी वज़ीर अलीखां से होना करार पा चुका है।’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book