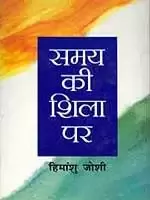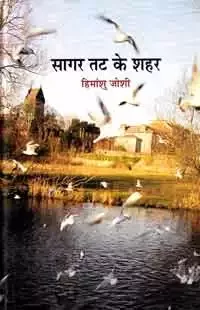|
नाटक-एकाँकी >> समय की शिला पर समय की शिला परहिमांशु जोशी
|
430 पाठक हैं |
||||||
इस नवीन कृति में आजादी के दीवानें, तीन देशभक्त क्रांतिकारियों पर नये अंदाज में लिखे रूपक हैं ।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
इस नवीन कृति में आजादी के दीवानें, तीन देशभक्त क्रांतिकारियों पर नये
अंदाज में लिखे रूपक हैं 1.नेताजी सुभाषचन्द्र बोस 2.फाँसी के तख्ते पर
हँसते हुए चढ़ जाने वाले अशफाक और 3.राष्ट्रनायक पं.गोविन्द वल्लभ पंत। इन
तीनों के व्यक्तित्व को चित्रित करती यह पुस्तक।
दो शब्द
अतीत ही नहीं होता इतिहास, कहीं वर्तमान भी होता है और भविषय भी। साए की
तरह वह समय के साथ-साथ निरन्तर चलता रहता है।
जब व्यक्ति नहीं रहता, समय भी बदल जाता है, तब भी साया रहता है—उसी रूप में, उसी तरह-पानी की सतह पर तिरती प्रतिच्छाया की भाँति !
जब इतिहास, यानी समय विशेष का दस्तावेज, सजीव होकर, चलचित्र की तरह उभर कर सामने आता है, तो कई अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर स्वयं सुलभ हो जाते हैं ! इतिहास तब मात्र मूक-दर्शक ही नहीं होता, वह सम आने पर बोलता भी है, चलता-ठिठकता भी। विश्व के सारे परिदृश्यों को अपनी दृष्टि में समा लेने की क्षमता भी रखता है। उसमें उभरती अमूर्त घटनाएं भी तब मूर्त होकर अपने अस्तित्व का अहसान जगाने लगती हैं।
लगभग समान काल-खण्डों में जिए तीन इतिहास पुरुषों की ये तीन जीवन-गाथाएँ मात्र एक सदी में समाई तीन सदियों की साक्षी हैं—राष्ट्र धर्म के निर्वाह में जिन्होंने अपने-अपने ढंग से अपनी आहुति दी।
परन्तु सुलझे हुए, दूरदर्शी राजनेता थे। स्वाधीनता-संग्राम के पुरोधा, नए भारत के निर्माता, गाँधी के अहिंसा के सिद्धांतों पर जिन की अटूट आस्था थी।
नेताजी एक धधकते अग्नि-पुंज की तरह भारत के क्षितिज पर उभरे ब्रिटिश शासकों ने अपने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी कि एक अकेला क्रान्तिकारी विश्व भर में फैले अंग्रेज़ी-साम्राज्वाद की जड़ें झकझोरकर रख देगा। और एक ऐसी चुनौती देगा, कि जिस साम्राज्य में कभी सूर्यास्त ही नहीं होता था, उसका सौभाग्य-सूर्य डूबता दिखलाई देगा।
‘तुम मुझे खून दो।
मैं तुम्हें आजादी दूँगा।’
पहली बार अंग्रेज़ों को अहसास हुआ कि ये धधकते शब्द एक अकेले व्यक्ति के नहीं, तीस करोड़ भारतीयों के कण्ठ से प्रस्फुटित होकर, वायु मण्डल को कँपा रहे हैं। आजादी की कीमत चुकाने के लिए जब कोई राष्ट्र उठ खड़ा होता है तो उसका मार्ग ईश्वर भी अवरुद्ध नहीं कर सकता।
‘आजाद हिन्द फौज’ का नेतृत्व करता हुआ एक सिंह-पुरुष, हाथ में तिरंगा फहराता हुआ, वर्मा की पहाड़ियों को रौंदता दहाड़ रहा था।
यह कैसी विडंबना थी। जब ब्रिटिश-साम्राज्यवाद का सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था—भारत की पूर्वी सीमाओं पर उगते सूरज का उजास बिखर रहा था।
स्वाधीनता की ज्वाला को और अधिक प्रज्वलित किया, क्रान्तिकारियों ने, अपने सिर पर कफन बाँध कर जो संग्राम में उतर आए थे। ये उभरते तरुण थे, जो आत्म-बलिदान के लिए तत्पर थे। उनमें अनेकत भगतसिंह थे। अनेक आजाद, अनेक सावरकर, अनेक चापेकर बन्धु, उनकी अनेक असफाक उल्ला खां, अनेक विस्मिल ! कालानी की कराल-कोठरियाँ, अनेक अन्तहीन शहादतों की साक्षी हैं।
इन तीनों की कार्य-प्रणालियाँ, जीवन-दर्शन भिन्न-भिन्न होते हुए भी कहीं पर्याप्त समानता थी। इनका प्रथम एवं अन्तिम लक्ष्य था—पराधीनता की बेड़ियाँ तोड़ कर मातृभूमि को मुक्त कराना।
पंडित पन्त, नेताजी तथा अशफाक उल्ला खां की जन्म-शताब्दियाँ-पंडित पन्त 10 सितम्बर 1987, नेताजी 23 जनवरी 1997, अशफाक उल्ला खाँ 23 अक्टूबर 1900 कुछ वर्ष पूर्व सारे देश में श्रद्धा के साथ मनाई गई। इनके जन्म दिन पर देश की सभी आकाशवाणी केन्द्रों से, देश की सभी प्रमुख भाषाओं में, एक साथ इन रूपकों में प्रसारित किया गया था—राष्ट्रीय प्रसारण के अन्तर्गत।
इनके लिए जहाँ-जहाँ जिन-जिन स्थानों में सम्भव हो पाया मैं गया। पन्तजी की जन्मभूमि खूँट-उत्तराँचल से होता हुआ, उनकी अन्तिम विश्रामस्थली 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली तक के अनेक पड़ाव पार किए। अल्मोड़ा की वह पाठशाला, जहाँ उन्होंने अक्षर-ज्ञान प्राप्त किया, इलाहाबाद का ‘मेकडोनल हिनम्दू होस्टल’ जिस के 112 नम्बर कमरे में पन्तजी रहते थे, अल्मोड़ा जेल, काशीपुर की अदालत, लखनऊ का मुख्यमन्त्री निवास आदि सभी स्थानों का परिभ्रमण किया। उन लोगों से भी मिला, जिन का पन्त जी से निकट का सम्बन्ध था।
इसी तरह उड़ीसा गया। कटक की वह इमारत देखी, जहाँ नेताजी का जन्म हुआ था। वह कॉलेज देखा, जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। कोलकाता वाला घर भी, जो अब संग्रहालय में परिवर्तित हो गया है। वह कार भी, जिस में बैठकर वे सरहद तक गए थे, जहाँ से पलायन कर उन्हें विदेश पहुँचना था।
अण्डमान, जहाँ उन्होंने भारत की मुक्त धरा पर पहली बार तिरंगा ध्वज फहराया था। मोराँग के मोर्चे को भी, जहाँ तक उन की सेना विजय-पताका फहराती हुई आई थी।
अशफाक तो एक जीवन्त किंवदंती रहे।
अशफाक का शहर शाहजहांपुर !
अशफाक का घर !
अशफाक की समाधि !
फैजाबाद का वह यातना-घर, जहाँ उन्हें फाँसी दी गई थी। ‘काकोरी ट्रेन काण्ड’ में चन्द्रशेखर आजाद के साथ ‘विस्मिल’, अशफाक, क्रान्तिकारी लेखक मन्थननाथ गुप्त भी थे, उन्हें उस छोटी उम्र में सोलह साल की सजा मिली थी ! ‘काकोरी-काण्ड’ में अशफाक की क्या भूमिका रही, विस्तार से गुप्त जी बतलाते हैं। सुखद आश्चर्य की बात है कि पन्तजी ने भी एक वकील के रूप में क्रान्तिकारियों की सहायता की थी। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचन्द्र भी एक मुकदमें की पैरवी के समय अदालत में आते थे। दर्शक-दीर्घा में सब से पीछे बैठ कर चुपचाप चले जाते थे।
न्यायाधीश ने जब अशफाक को दो बार फाँसी की सजा दो बार कालापानी का दण्ड सुनाया तो असफाक उसकी खिल्ली उड़ाते हुए हँसने लगे थे। उन्होंने कहा था, ‘‘यह मेरी खुश-किस्मती है कि ब्रिटिश हुकूमत ने इतनी बड़ी सजाएँ देकर इन्कलाबी के रूप में मुझे इज्जत बख्शी है। मैं उनका तहेदिल से शुक्र गुजार हूँ।’’
कम लोग जानते हैं कि जेल में काल-कोठरी में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की तरह अशफाक उल्ला खाँ ने भी फाँसी से पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी। उस विस्मृत ग्रन्थ को भी ढूँढ़ा। उसके फटे हुए पीले पन्ने भी पलटे।
देश की आजादी केवल गाँधी जी के अहिंसक मार्ग से ही नहीं मिली, उसमें अमर शहीद भगतसिंह जैसे क्रान्तिकारियों तथा नेताजी जैसे सैन्यबल पर आस्था रखने वाले देशभक्तों का भी योगदान रहा।
रेडियो-रूपक विधा के विशेषज्ञ भाई डॉ. वीरेन्द्र गोहिल को इन रूपकों को लिखाने का श्रेय जाता है, यदि वे पीछे पड़ कर न लिखवाते तो सम्भवतः ये लिखे ही नहीं जाते।
समय की शिला पर अंकित, शहीदों के जीवन्त इतिहास के ये कुछ प्रेरक पृष्ठ यदि नई पीढ़ी में यह अहसास जगाने में सफल रहे कि यह आजादी यों ही नहीं मिल गई थी, इसके लिए कितने देश भक्तों ने बलिदान दिए-तो अपना यह विनम्र प्रयास सार्थक समझूँगा।
जब व्यक्ति नहीं रहता, समय भी बदल जाता है, तब भी साया रहता है—उसी रूप में, उसी तरह-पानी की सतह पर तिरती प्रतिच्छाया की भाँति !
जब इतिहास, यानी समय विशेष का दस्तावेज, सजीव होकर, चलचित्र की तरह उभर कर सामने आता है, तो कई अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर स्वयं सुलभ हो जाते हैं ! इतिहास तब मात्र मूक-दर्शक ही नहीं होता, वह सम आने पर बोलता भी है, चलता-ठिठकता भी। विश्व के सारे परिदृश्यों को अपनी दृष्टि में समा लेने की क्षमता भी रखता है। उसमें उभरती अमूर्त घटनाएं भी तब मूर्त होकर अपने अस्तित्व का अहसान जगाने लगती हैं।
लगभग समान काल-खण्डों में जिए तीन इतिहास पुरुषों की ये तीन जीवन-गाथाएँ मात्र एक सदी में समाई तीन सदियों की साक्षी हैं—राष्ट्र धर्म के निर्वाह में जिन्होंने अपने-अपने ढंग से अपनी आहुति दी।
परन्तु सुलझे हुए, दूरदर्शी राजनेता थे। स्वाधीनता-संग्राम के पुरोधा, नए भारत के निर्माता, गाँधी के अहिंसा के सिद्धांतों पर जिन की अटूट आस्था थी।
नेताजी एक धधकते अग्नि-पुंज की तरह भारत के क्षितिज पर उभरे ब्रिटिश शासकों ने अपने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी कि एक अकेला क्रान्तिकारी विश्व भर में फैले अंग्रेज़ी-साम्राज्वाद की जड़ें झकझोरकर रख देगा। और एक ऐसी चुनौती देगा, कि जिस साम्राज्य में कभी सूर्यास्त ही नहीं होता था, उसका सौभाग्य-सूर्य डूबता दिखलाई देगा।
‘तुम मुझे खून दो।
मैं तुम्हें आजादी दूँगा।’
पहली बार अंग्रेज़ों को अहसास हुआ कि ये धधकते शब्द एक अकेले व्यक्ति के नहीं, तीस करोड़ भारतीयों के कण्ठ से प्रस्फुटित होकर, वायु मण्डल को कँपा रहे हैं। आजादी की कीमत चुकाने के लिए जब कोई राष्ट्र उठ खड़ा होता है तो उसका मार्ग ईश्वर भी अवरुद्ध नहीं कर सकता।
‘आजाद हिन्द फौज’ का नेतृत्व करता हुआ एक सिंह-पुरुष, हाथ में तिरंगा फहराता हुआ, वर्मा की पहाड़ियों को रौंदता दहाड़ रहा था।
यह कैसी विडंबना थी। जब ब्रिटिश-साम्राज्यवाद का सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था—भारत की पूर्वी सीमाओं पर उगते सूरज का उजास बिखर रहा था।
स्वाधीनता की ज्वाला को और अधिक प्रज्वलित किया, क्रान्तिकारियों ने, अपने सिर पर कफन बाँध कर जो संग्राम में उतर आए थे। ये उभरते तरुण थे, जो आत्म-बलिदान के लिए तत्पर थे। उनमें अनेकत भगतसिंह थे। अनेक आजाद, अनेक सावरकर, अनेक चापेकर बन्धु, उनकी अनेक असफाक उल्ला खां, अनेक विस्मिल ! कालानी की कराल-कोठरियाँ, अनेक अन्तहीन शहादतों की साक्षी हैं।
इन तीनों की कार्य-प्रणालियाँ, जीवन-दर्शन भिन्न-भिन्न होते हुए भी कहीं पर्याप्त समानता थी। इनका प्रथम एवं अन्तिम लक्ष्य था—पराधीनता की बेड़ियाँ तोड़ कर मातृभूमि को मुक्त कराना।
पंडित पन्त, नेताजी तथा अशफाक उल्ला खां की जन्म-शताब्दियाँ-पंडित पन्त 10 सितम्बर 1987, नेताजी 23 जनवरी 1997, अशफाक उल्ला खाँ 23 अक्टूबर 1900 कुछ वर्ष पूर्व सारे देश में श्रद्धा के साथ मनाई गई। इनके जन्म दिन पर देश की सभी आकाशवाणी केन्द्रों से, देश की सभी प्रमुख भाषाओं में, एक साथ इन रूपकों में प्रसारित किया गया था—राष्ट्रीय प्रसारण के अन्तर्गत।
इनके लिए जहाँ-जहाँ जिन-जिन स्थानों में सम्भव हो पाया मैं गया। पन्तजी की जन्मभूमि खूँट-उत्तराँचल से होता हुआ, उनकी अन्तिम विश्रामस्थली 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली तक के अनेक पड़ाव पार किए। अल्मोड़ा की वह पाठशाला, जहाँ उन्होंने अक्षर-ज्ञान प्राप्त किया, इलाहाबाद का ‘मेकडोनल हिनम्दू होस्टल’ जिस के 112 नम्बर कमरे में पन्तजी रहते थे, अल्मोड़ा जेल, काशीपुर की अदालत, लखनऊ का मुख्यमन्त्री निवास आदि सभी स्थानों का परिभ्रमण किया। उन लोगों से भी मिला, जिन का पन्त जी से निकट का सम्बन्ध था।
इसी तरह उड़ीसा गया। कटक की वह इमारत देखी, जहाँ नेताजी का जन्म हुआ था। वह कॉलेज देखा, जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। कोलकाता वाला घर भी, जो अब संग्रहालय में परिवर्तित हो गया है। वह कार भी, जिस में बैठकर वे सरहद तक गए थे, जहाँ से पलायन कर उन्हें विदेश पहुँचना था।
अण्डमान, जहाँ उन्होंने भारत की मुक्त धरा पर पहली बार तिरंगा ध्वज फहराया था। मोराँग के मोर्चे को भी, जहाँ तक उन की सेना विजय-पताका फहराती हुई आई थी।
अशफाक तो एक जीवन्त किंवदंती रहे।
अशफाक का शहर शाहजहांपुर !
अशफाक का घर !
अशफाक की समाधि !
फैजाबाद का वह यातना-घर, जहाँ उन्हें फाँसी दी गई थी। ‘काकोरी ट्रेन काण्ड’ में चन्द्रशेखर आजाद के साथ ‘विस्मिल’, अशफाक, क्रान्तिकारी लेखक मन्थननाथ गुप्त भी थे, उन्हें उस छोटी उम्र में सोलह साल की सजा मिली थी ! ‘काकोरी-काण्ड’ में अशफाक की क्या भूमिका रही, विस्तार से गुप्त जी बतलाते हैं। सुखद आश्चर्य की बात है कि पन्तजी ने भी एक वकील के रूप में क्रान्तिकारियों की सहायता की थी। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचन्द्र भी एक मुकदमें की पैरवी के समय अदालत में आते थे। दर्शक-दीर्घा में सब से पीछे बैठ कर चुपचाप चले जाते थे।
न्यायाधीश ने जब अशफाक को दो बार फाँसी की सजा दो बार कालापानी का दण्ड सुनाया तो असफाक उसकी खिल्ली उड़ाते हुए हँसने लगे थे। उन्होंने कहा था, ‘‘यह मेरी खुश-किस्मती है कि ब्रिटिश हुकूमत ने इतनी बड़ी सजाएँ देकर इन्कलाबी के रूप में मुझे इज्जत बख्शी है। मैं उनका तहेदिल से शुक्र गुजार हूँ।’’
कम लोग जानते हैं कि जेल में काल-कोठरी में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की तरह अशफाक उल्ला खाँ ने भी फाँसी से पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी। उस विस्मृत ग्रन्थ को भी ढूँढ़ा। उसके फटे हुए पीले पन्ने भी पलटे।
देश की आजादी केवल गाँधी जी के अहिंसक मार्ग से ही नहीं मिली, उसमें अमर शहीद भगतसिंह जैसे क्रान्तिकारियों तथा नेताजी जैसे सैन्यबल पर आस्था रखने वाले देशभक्तों का भी योगदान रहा।
रेडियो-रूपक विधा के विशेषज्ञ भाई डॉ. वीरेन्द्र गोहिल को इन रूपकों को लिखाने का श्रेय जाता है, यदि वे पीछे पड़ कर न लिखवाते तो सम्भवतः ये लिखे ही नहीं जाते।
समय की शिला पर अंकित, शहीदों के जीवन्त इतिहास के ये कुछ प्रेरक पृष्ठ यदि नई पीढ़ी में यह अहसास जगाने में सफल रहे कि यह आजादी यों ही नहीं मिल गई थी, इसके लिए कितने देश भक्तों ने बलिदान दिए-तो अपना यह विनम्र प्रयास सार्थक समझूँगा।
हिमांशु जोशी
शब्द-चित्रों का अनूठा संसार
‘रेडियो रूपक’ प्रसारण की एक अद्भुत विधा है। अद्भुत
इसलिए कि
इसके लेखन और प्रस्तुति में रेडियो प्रसारण की सभी विधाओं का समावेश हो
सकता है। जिसे संगीत, नाटक, इन्टरव्यू, परिचर्चा, रिर्पोताज, समाचार,
आँखों देखा हाल, न्य़ूज रील, कम्पेयरिंग, यात्रा-वृत्तान्त कविता, गीत,
कहानी, संवाद, नरेशन आदि आदि। इसीलिए विशेषज्ञों ने रेडियो रूपक को भी
‘सभी विधाओं की विधा’ कहा है। इसके लेखन और प्रस्तुति
को
सीमाओं में नहीं बाँधा जा सकता। असीम है रूपक का संसार।
‘विद्युत चुम्बकीय तरंगों तथा रेडियो संचार’ का आविष्कार बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में हो गया था। शुरू-शुरू में विज्ञान के इन महान आविष्कारों का इस्तेमाल तूफानों में फँसे नाविक प्रायः अपनी सुरक्षा की पुकार अन्य लोगों तक पहुँचाने के लिए करते थे। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान गुप्त सूचनाओं से लेकर प्रोपेगंडा तक का काम इस माध्यम की उपयोगिता से जुड़ा। 1916 में विश्व का पहला रेडियो समाचार प्रसारित हुआ। दुनिया ने रेडियो की असीम शक्ति को पहचाना। 1919 में अमेरिका में एक निगम की स्थापना हुई और 21 दिसम्बर, 1922 को विश्व के पहले रेडियो प्रसारण का जन्म हु्आ। ब्रिटेन में सन 1922 में बी.बी.सी. की स्थापना हुई। भारत में 23 जुलाई, 1927 से रेडियो का नियमित प्रसारण शुरू हुआ।
रेडियो के जन्म से पहले से ही साहित्य और संचार की अनेक विधाएँ विद्यमान थीं। लेकिन रूपक विधा नहीं थी। रूपक का जन्म रेडियो के जन्म के बाद हुआ। रूपक को आम तौर पर ‘डाक्यूमेंटरी फीचर’ के नाम से जाना जाता है। विश्वप्रसिद्ध प्रसारणकर्ता श्री जान गिरसन ने सन् 1926 में सबसे पहली बार ‘डाक्युमेंटरी’ शब्द का प्रयोग किया। डाक्युमेंटरी शब्द मूलरूप से फ्रेंच भाषा से लिया गया है। फ्रेंच भाषा में इसे ‘दाक्यूमेंतायर’ कहा जाता है। इसका अर्थ—यात्रा-वृत्तान्त। लेकिन ऐसा वृत्तान्त जो तथ्यों से परिपूर्ण है। गिरसन ने कहा—यह जानकारी बाले शब्द चित्र।
हर माध्यम की अपनी आवश्कताएँ होती हैं, अपनी विशेषताएँ और होती हैं अपनी सीमाएँ। रेडियो की पहली विशेषता है कि इसे केवल सुना जा सकता है। इसलिए इसकी भाषा बोलने वाली भाषा है। इसके लिए प्रयोग में लाने वाले शब्द वही हैं जो सुनने वालों को आसानी से समझ में आ जायें। इसकी पहली आवश्यकता है कि इसके श्रोताओं के बारे में सम्पूर्ण जानकारी। श्रोता ग्राहक की तरह हैं। इसके अदृश्य श्रोताओं का मासिक, शैक्षणिक, भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का अध्ययन किए बिना प्रभावशाली और उपयोगी प्रसारण लेखन नहीं हो सकता। इसलिए रेडियो ने एक नए साहित्य को जन्म दिया। नया आयाम दिया। श्रव्य-साहित्य।
जिस तरह हर अध्यापक साहित्यकार नहीं हो सकता भले ही वह साहित्य का अध्यापन ही क्यों न करता हो ! जिस पर वह पत्रकार जन-संचार के सभी माध्यमों के लिए उपयोगी लेखन करने में सक्षम नहीं होता, उसी तरह हर साहित्यकार अच्छा पत्रकार नहीं हो सकता। क्योंकि हर विधा की अपनी मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं। रेडियो प्रसारण के लिए किसी भी विधा के आलेख लिखते समय अलग किस्म की भाषा, शब्दावली, प्रतीक, अदृश्य श्रोताओं के लिए शब्द चित्र बनाने की कला, एक विशेष प्रकार की रवानगी से परिचय, रिद्म, शिल्प सौन्दर्य, नीरस विषयों और जानकारी वाले सन्दर्भों को सरस, मनोरंजक और सजीव बनाने की कला में निपुणता परम आवश्यक है।
रेडियों प्रसारण के लिए लेखन के बारे में कहा जाता है कि यह जानना जरूरी नहीं है कि आपको कहना है, बल्कि यह जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि किसके लिए कहना है (आपका श्रोता कौन है), लोकप्रिय और बहुपोगी विधा रूपक को पूरी तरह बिना अभ्यास के नहीं जाना जा सकता। जिस तरह तालाब या नदी के किनारे बैठकर, कुछ किताबें पढ़कर या प्रशिक्षक से ज्ञान प्राप्त करके तैरना नहीं सीखा जा सकता, उसी तरह रूपक को भी नहीं जाना जा सकता। तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना ही होगा, उसी तरह रूपक विधा का जनाकार होने के लिए रूपक को सुनना, समझना और अभ्यास करना अनिवार्य होता है। ऐसे बिरले ही साहित्यकार—पत्रकार होते हैं जो प्रसारण माध्यमों की विभिन्न विधाओं में समान रूप से सक्षमतापूर्वक लिखने की कला जानते हैं। यह चुनौती भरा काम माना जाता है।
‘विद्युत चुम्बकीय तरंगों तथा रेडियो संचार’ का आविष्कार बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में हो गया था। शुरू-शुरू में विज्ञान के इन महान आविष्कारों का इस्तेमाल तूफानों में फँसे नाविक प्रायः अपनी सुरक्षा की पुकार अन्य लोगों तक पहुँचाने के लिए करते थे। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान गुप्त सूचनाओं से लेकर प्रोपेगंडा तक का काम इस माध्यम की उपयोगिता से जुड़ा। 1916 में विश्व का पहला रेडियो समाचार प्रसारित हुआ। दुनिया ने रेडियो की असीम शक्ति को पहचाना। 1919 में अमेरिका में एक निगम की स्थापना हुई और 21 दिसम्बर, 1922 को विश्व के पहले रेडियो प्रसारण का जन्म हु्आ। ब्रिटेन में सन 1922 में बी.बी.सी. की स्थापना हुई। भारत में 23 जुलाई, 1927 से रेडियो का नियमित प्रसारण शुरू हुआ।
रेडियो के जन्म से पहले से ही साहित्य और संचार की अनेक विधाएँ विद्यमान थीं। लेकिन रूपक विधा नहीं थी। रूपक का जन्म रेडियो के जन्म के बाद हुआ। रूपक को आम तौर पर ‘डाक्यूमेंटरी फीचर’ के नाम से जाना जाता है। विश्वप्रसिद्ध प्रसारणकर्ता श्री जान गिरसन ने सन् 1926 में सबसे पहली बार ‘डाक्युमेंटरी’ शब्द का प्रयोग किया। डाक्युमेंटरी शब्द मूलरूप से फ्रेंच भाषा से लिया गया है। फ्रेंच भाषा में इसे ‘दाक्यूमेंतायर’ कहा जाता है। इसका अर्थ—यात्रा-वृत्तान्त। लेकिन ऐसा वृत्तान्त जो तथ्यों से परिपूर्ण है। गिरसन ने कहा—यह जानकारी बाले शब्द चित्र।
हर माध्यम की अपनी आवश्कताएँ होती हैं, अपनी विशेषताएँ और होती हैं अपनी सीमाएँ। रेडियो की पहली विशेषता है कि इसे केवल सुना जा सकता है। इसलिए इसकी भाषा बोलने वाली भाषा है। इसके लिए प्रयोग में लाने वाले शब्द वही हैं जो सुनने वालों को आसानी से समझ में आ जायें। इसकी पहली आवश्यकता है कि इसके श्रोताओं के बारे में सम्पूर्ण जानकारी। श्रोता ग्राहक की तरह हैं। इसके अदृश्य श्रोताओं का मासिक, शैक्षणिक, भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का अध्ययन किए बिना प्रभावशाली और उपयोगी प्रसारण लेखन नहीं हो सकता। इसलिए रेडियो ने एक नए साहित्य को जन्म दिया। नया आयाम दिया। श्रव्य-साहित्य।
जिस तरह हर अध्यापक साहित्यकार नहीं हो सकता भले ही वह साहित्य का अध्यापन ही क्यों न करता हो ! जिस पर वह पत्रकार जन-संचार के सभी माध्यमों के लिए उपयोगी लेखन करने में सक्षम नहीं होता, उसी तरह हर साहित्यकार अच्छा पत्रकार नहीं हो सकता। क्योंकि हर विधा की अपनी मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं। रेडियो प्रसारण के लिए किसी भी विधा के आलेख लिखते समय अलग किस्म की भाषा, शब्दावली, प्रतीक, अदृश्य श्रोताओं के लिए शब्द चित्र बनाने की कला, एक विशेष प्रकार की रवानगी से परिचय, रिद्म, शिल्प सौन्दर्य, नीरस विषयों और जानकारी वाले सन्दर्भों को सरस, मनोरंजक और सजीव बनाने की कला में निपुणता परम आवश्यक है।
रेडियों प्रसारण के लिए लेखन के बारे में कहा जाता है कि यह जानना जरूरी नहीं है कि आपको कहना है, बल्कि यह जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि किसके लिए कहना है (आपका श्रोता कौन है), लोकप्रिय और बहुपोगी विधा रूपक को पूरी तरह बिना अभ्यास के नहीं जाना जा सकता। जिस तरह तालाब या नदी के किनारे बैठकर, कुछ किताबें पढ़कर या प्रशिक्षक से ज्ञान प्राप्त करके तैरना नहीं सीखा जा सकता, उसी तरह रूपक को भी नहीं जाना जा सकता। तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना ही होगा, उसी तरह रूपक विधा का जनाकार होने के लिए रूपक को सुनना, समझना और अभ्यास करना अनिवार्य होता है। ऐसे बिरले ही साहित्यकार—पत्रकार होते हैं जो प्रसारण माध्यमों की विभिन्न विधाओं में समान रूप से सक्षमतापूर्वक लिखने की कला जानते हैं। यह चुनौती भरा काम माना जाता है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book