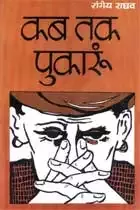|
सामाजिक >> कब तक पुकारूं कब तक पुकारूंरांगेय राघव
|
44 पाठक हैं |
||||||
रांगेय राघव की प्रतिभा और लेखन-क्षमता को अभिषिक्त करने वाली जीवंत औपन्यासिक रचना...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
परिचय : डॉ. रांगेय राघव
17 जनवरी, 1923 को जन्म आगरा में। मूलनाम टी.एन.वी. आचार्य (तिरुमल्लै
नम्बाकम् वीर राघव आचार्य)। कुल से दक्षिणात्य लेकिन ढाई शतक से पूर्वज
वैर (भरतपुर) के निवासी और वैर बारोनी गाँवों के जागीरदार। घर की बोली
बृज, तमिल।
शिक्षा आगरा में। सेंट जॉन्स कालेज से 1944 में स्नातकोत्तर और 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से गुरु गोरखनाथ पर पी.एच.डी.। हिंदी, अंग्रेजी, बृज और संस्कृत पर असाधारण अधिकार।
13 वर्ष की आयु में लेखनारंभ। 23-24 वर्ष की आयु में ही अभूतपूर्व चर्चा के विषय। 1942 में अकालग्रस्त बंगाल यात्रा के बाद लिखे रिपोर्तराज ‘तूफानों के बीच’ लिखकर हिंदी में रिपोर्तराज विद्या को जन्म देने वालों में अग्रणी।
साहित्य के अतिरिक्त चित्रकला, संगीत और पुरातत्व में विशेष रुचि। साहित्य की प्रायः सभी विद्याओं में सिद्धहस्त। मात्र 39 वर्ष की आयु में साहित्य को कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्तराज के अतिरिक्त आलोचना, सभ्यता और संस्कृति पर शोध व व्याख्या के क्षेत्रों की 150 से भी अधिक पुस्तकों से समृद्ध-किया। अपनी अद्भुत प्रतिभा, असाधारण ज्ञान और लेखन क्षमता के लिए सर्वमान्य अद्वितीय लेखक।
संस्कृत रचनाओं का हिंदी, अंग्रेजी में अनुवाद। विदेशी साहित्य का हिंदी में अनुवाद। देशी-विदेशी साहित्य का पुनर्लेखन।
7 मई, 1956 को सुलोचना जी से विवाह। 8 फरवरी, 1960 को पुत्री-सीमन्तिनी का जन्म। अधिकांश जीवन आगरा, वैर और जयपुर में व्यतीत। आजीवन स्वतंत्र लेखन।
हिन्दुस्तानी अकादमी पुरस्कार (1951), डालमिया पुरस्कार (1954), उत्तर प्रदेश सरकार पुरस्कार (1957 व 1959), राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार (1961) तथा मरणोपरान्त (1966) महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित।
अनेकों कृतियां अन्य भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुदित और प्रशंसित।
लम्बी बीमारी के बाद 12 सितम्बर, 1962 को बंबई में देहान्त।
शिक्षा आगरा में। सेंट जॉन्स कालेज से 1944 में स्नातकोत्तर और 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से गुरु गोरखनाथ पर पी.एच.डी.। हिंदी, अंग्रेजी, बृज और संस्कृत पर असाधारण अधिकार।
13 वर्ष की आयु में लेखनारंभ। 23-24 वर्ष की आयु में ही अभूतपूर्व चर्चा के विषय। 1942 में अकालग्रस्त बंगाल यात्रा के बाद लिखे रिपोर्तराज ‘तूफानों के बीच’ लिखकर हिंदी में रिपोर्तराज विद्या को जन्म देने वालों में अग्रणी।
साहित्य के अतिरिक्त चित्रकला, संगीत और पुरातत्व में विशेष रुचि। साहित्य की प्रायः सभी विद्याओं में सिद्धहस्त। मात्र 39 वर्ष की आयु में साहित्य को कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्तराज के अतिरिक्त आलोचना, सभ्यता और संस्कृति पर शोध व व्याख्या के क्षेत्रों की 150 से भी अधिक पुस्तकों से समृद्ध-किया। अपनी अद्भुत प्रतिभा, असाधारण ज्ञान और लेखन क्षमता के लिए सर्वमान्य अद्वितीय लेखक।
संस्कृत रचनाओं का हिंदी, अंग्रेजी में अनुवाद। विदेशी साहित्य का हिंदी में अनुवाद। देशी-विदेशी साहित्य का पुनर्लेखन।
7 मई, 1956 को सुलोचना जी से विवाह। 8 फरवरी, 1960 को पुत्री-सीमन्तिनी का जन्म। अधिकांश जीवन आगरा, वैर और जयपुर में व्यतीत। आजीवन स्वतंत्र लेखन।
हिन्दुस्तानी अकादमी पुरस्कार (1951), डालमिया पुरस्कार (1954), उत्तर प्रदेश सरकार पुरस्कार (1957 व 1959), राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार (1961) तथा मरणोपरान्त (1966) महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित।
अनेकों कृतियां अन्य भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुदित और प्रशंसित।
लम्बी बीमारी के बाद 12 सितम्बर, 1962 को बंबई में देहान्त।
1949 ई. की बात है।
उन दिनों मैं गाँव में रहता था। मैं अस्वस्थ रहा करता था। जिस स्थान पर
मैं रहता था, वहां एक नीरवता छायी रहती और दिन में कभी-कभी गायें और
भैंसें वहां पेड़ों की छाया में बैठकर जुगाली किया करतीं। सब अपने-अपने
धन्धों में लगे रहते। पेड़ों की छाया घनी-घनी-सी जब पूस की ठंडी हवाओं में
कांपती, तब धूप बहुत ही अच्छी लगती। मेरे पांव का फोड़ा अब अच्छा होने लगा
था। वह ऐसा भयानक था कि मैं शहर के लगभग सभी डॉक्टरों को आज़मा चुका था।
हकीम साहब के काढ़े, एलोपैथ की नुकीली सुइयां, होम्योपैथों के पानी के घोल
उस पर व्यर्थ हो गए, तो मुझे एक आदमी ने राय दी और मैं यहां चला आया। दूर
तक यहां झील झाईं मारती, हवा के थपेड़ों में ऐसी लहर मारती कि जैसे कोई
झीनी चादर सरकती चली जा रही हो और अब वह उठ जाएगी, उठ जाएगी, पर ऐसा नहीं
होता। मैं देर तक उसे देखा करता।
मेरा इलाजी एक और भी आश्चर्यजनक व्यक्ति था। वह गले में मालाएं पहनता, सिर पर साफा बांधे रहता और हाथों में कांच के कड़े पहनता। वह इतने पुराने युग का था और मैं अपने को नितान्त आधुनिकता समझता था। मैं कभी इन गंवार इलाजों में भरोसा नहीं करता, पर त ही कुछ ऐसी पड़ गई कि मुझे झुकना पड़ गया। वह जंगल से रुखड़ी तोड़कर लाता, किसी को उसके बारे में नहीं बताता, पर मेरे सामने बैठकर जादू-सा करता। कभी उसमें फूंक मारता, कभी आंखें फाड़कर आसमान की तरफ देखता और कभी झूमर-सी मारता हुआ चटाचट आवाज़ करके अपनी अंगुलियां चटकाता। मैं सब समझता था कि ये सब इसके मध्यकालीन अंधविश्वास हैं। परंतु वह एक दिन इस बात पर नाराज हो गया। उसने कहा कि वह किसीके भी सामने यह रूखड़ी खोलने की बात नहीं करता, पर क्योंकि मैं शहरी हूं, इसलिए उसने इसमें कोई डर महसूस नहीं किया। उसने मुस्कराकर कहा : बाबू ! तुम बिलिया और बैंगन के पत्ते का फरक नहीं जानते, फिर तुमसे क्या डर !’
उसके स्वर में कहीं व्यंग्य था जैसा हम शहरी लोगों में गांववालों के प्रति होता है।
मैं मुस्कराया। तब उसने चिढ़कर कहा : ‘बाबू भैया ! तुम तो फिर भी अपने हो, मेरी इस रूखड़ी पर जब मन्तर डोला था तब साब अजंट थर्रा गया था।’
अब मेरे कान ज़रा खड़े हुए।
‘सो कैसे ?’ मैंने पूछा। और आज पहली बार मैंने उसके मुख की ओर देखा। साफे, मूंछों और गाय की धूल ने उसको ढंक लिया था। उसका रंग तांबे की तरह तपा हुआ था। आंखों में एक चमक थी। अब वह लगभग चालीस बरस का हो गया था। उसकी सीधी लम्बी नाक बड़ी सुन्दर थी। वह एक घुटने तक की धोती और कुछ लम्बा-सा खुले गले का कोट पहने था। और मैंने कल्पना की कि एक दिन वह सुखराम नट चौड़ी हड्डियों का गबरू जवान रहा होगा। उसकी आंखें बहुत सुन्दर रही होंगी, जिसके दोनों ओर अब गोल लकीरें खिंच गई थीं।
उस दिन वह चला गया।
सातवें दिन उसने पट्टी खोल दी और कहा : ‘आज बाबू भैया, मेरे संग घूमने चलो। तुम्हें अपनी दवाई का जादू दिखाऊँगा। ‘मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा—ज़रूर इन रूखड़ियों की वैज्ञानिक खोज होनी चाहिए। पर मुसीबत तो यह है कि वे लोग गुरु-परंपरा से पायी हुई इन चीज़ों को हवा तक नहीं देते। सदियों से जो काम हो चुका है, उसको ये लोग ईश्वरीय समझकर उसे सुलझाने के बजाय धार्मिक और दैवी बनाकर उलझाने में ही अपना गौरव समझते हैं।
आज हम लोग घूमने थोड़ी ही दूर गए। फुलवारी में बैठे रहे। उसके बीचोंबीच एक सफेद महल था। मैंने पूछा : ‘यह कब का बना है ?’
सुखराम ने कहा : ‘जब इस राजा की अमलदारी शुरू हुई थी, तब पहले राजा ने इसे बनवाया था।’
महल सुन्दर था। जाड़े की शाम। डूबते सूरज की किरणें बेरों के सुगन्धित जंगल पर पड़कर अमलतासों और सेमल के पेड़ों पर फिसल रही थी। और फिर कच्चे दगरे की गाय-भैंसों के खुरों से उठी धूल पर आर पार हो जाने का प्रयत्न कर रही थीं। चारों ओर ठंडक थी। दूर एक पेड़ के नीचे हनुमान जी थे, लाल सिन्दूर में लगे; और एक पहलवान नंगे बदन, अखाड़े की मिट्टी को मले हुए, लंगोट बांधे, दनादन बैठक लगा रहा था। एकमात्र कमरख के फलहीन पेड़ के सामने वह मुझे बड़ा अजीब-सा लग रहा था।
गांव की शाम की गंदगी, परेशानी सब धीरे-धीरे उतरते अंधेरे में छिपती चली जा रही थी और चारों ओर लौटते पक्षियों का कलरव अंधेरे के पावों के नीचे तिरता-तिरता दबा जा रहा था। मन्दिरों की झालरों और घंटो की आवाज़ अब ऐसी सुनायी देती थी जैसे किसी ने तांता जोड़ दिया हो। और दूर बजती बैलों की घंटियां और भी एक सूनापन भर-भर देती थीं।
सुखराम ने कहा : ‘कल और आगे चलेंगे।’
मैंने कहा : ‘वह क्या है ?’
सुखराम ने कहा : ‘रोज तो देखते ही हो।’
मैंने कहा : ‘किला है। किसने बनवाया था ?’
सुखराम ने उत्तर दिया :‘उसी राजा के बेटे ने।’
मैंने कहा : ‘छोटा ही है।’
‘रह गया है।’
मैंने पूछा :‘क्या मतलब ?’
‘‘अधूरा किला है।’
‘शायद राजा मर गया था ?’
‘हां, बाबू भैया। कहते हैं, राज्य के लिए उसकी भाभी ने उसे ज़हर दे दिया था। वह जानते हुए पी गया था।’
कहते हुए सुखराम की आंखों में पानी छलक आया। मैं समझा नहीं। मैंने कहा : ‘ऐसा क्यों हुआ सुखराम ? और इससे तुम्हें रोने की क्या त है ?’
वह आंसू पोंछकर मुस्कराया। उसने कहा : ‘कुछ नहीं बाबू भैया ! अब जमाना बदल गया है। राजाओं के ही राज चले गए तो इन बातों से फायदा ही क्या है !’
‘नहीं, नहीं सुखराम’, मेरे भिखारी उपन्यासकार ने याचना की, ‘बताओ न ! मैं तो परदेसी हूं। उस दिन तुम साहब के थर्राने की बात कहते-कहते रुक गए थे, आज तुम इस बात को भी छिपा रहे हो।’
परन्तु वह कुछ नहीं बोला। उसने बात बदलकर कहा : ‘क्यों, अब चल सकते हो न ?’
‘क्यों नहीं। कल और भी चलेंगे।’
‘हां, अब क्या डर है ?’
‘सुखराम, वह क्या है ?’ मैंने एक ओर हाथ उठाकर कहा।
वह एक नीला पहाड़ था। उसपर एक गहरा सन्नाटा था। लगता था, आसमान से उतरता अंधेरा पहले वहां इकट्ठा हो गया है और अब हवा के झोंके उसीसे उड़ा-उड़ाकर उसे इधर-उधर फैला रहे हैं। सुखराम ने कहा : ‘चलो बाबू भैया ! चलो।’
उसने जैसे मेरी बांसुरी में से तरह-तरह के राग निकलते देखकर किसी भी राग को पकड़ने की जगह बांसुरी के रंध्र को ही उंगली से दबाकर बन्द कर दिया। मेरी सारी जिज्ञासा रुंधी हुई पड़ी रह गई।
तीसरे दिन जब हम लोग जंगल में पहुंचे तो सामने धुंआ उठता हुआ दिखायी दिया। मैंने कहा : ‘यह क्या है ?’
‘यह हमारी बस्ती है।’ सुखराम ने कहा।
मैंने देखा, छोटे-छोटे घर थे। और अब सांझ उस जंगल से बस्ती को चारों ओर से घिराव डालकर दबाए ले रही थी। शायद ही दस घर हों। मैंने सोचा—यह संसार कितनी तरह का है ? कहीं बम्बई की भीड़, कहीं आदमी ऐसे भी सन्नाटे में रहकर उम्र गुज़ार देता है ? सामने एक बड़ा-सा कुआं था। मैं उसकी ओर बढ़ा, पर वहां पहुंच कर ठिठक गया। एक बच्ची, लगभग तेरह या चौदह वर्ष की, वहां पानी खींच रही थी; वह ऊंचा घाघरा और फरिया पहने थी। फरिया इस वक़्त उसके कंधों के नीचे पड़ी थी। उसकी ओर मैंने देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ। उसके नेत्र नीले, बाल सुनहले और रंग भभूका सफेद था। उसकी नाक कुछ आगे उठी हुई थी और उसके गालों पर सुर्खी थी। वह मुस्करायी।
‘कौन ?’ सुखराम ने कहा : ‘चन्दा, अभी घर नहीं गई ?’
‘रोटी बनाकर धर आई हूं दादा (पिता), पानी का एक डोल लेने आई थी।’
मुझे अब मालूम हुआ कि वह सुखराम की बेटी थी। परन्तु कितना अजीब था। वह लड़की बिलकुल अंग्रेज मालूम देती थी। उसकी आवाज़ में कितना तीखा पतलापन था कि मेरा विश्वास विचलित हो उठा।
सुखराम ने बीड़ी सुलगा ली और फिर ध्यान में डूब गया। मैं सोच नहीं सका। सामने पहाड़ के पैरों पर चांदी की बेड़ी-सी एक इमारत खड़ी थी। मैंने उसकी ओर इशारा करके पूछा : ‘सुखराम, वह क्या है ?’
लड़की ने हंसकर कहा :‘डाक बंगला। पहले यहां सा’ब लोग आया करते थे। अब तो उनका राज ही चला गया।’
वह फिर हंसी और सुखराम की आंखों में एक छाया-सी डबडबा आई, कातर, परन्तु अर्निद्य, सुखावह नहीं, अपने-आप में पूर्ण।
उस दिन और बात नहीं हुई। मैं घर आ गया। जिनके घर ठहरा था, वे मित्र खाने के समय यह बताने में लगे रहे कि अब वे नई जिन्दगी शुरू करना चाहते थे। उनका दिल गांव से ऊब गया था। बड़ी देर तक वे गांव की निंदा करते रहे, परंतु उन्होंने सारांश यही निकाला कि गांव हर हालत में शहर से अच्छा होता है, अतः वे यहीं रहेंगे। मेरे पांव की बात चली। फिर सुखराम की बात आई। मैंने उसकी लड़की के बारे में भी ज़िक्र किया। मेरे दोस्त ने हुक्का पास सरकाया और खाने की थाली में हाथ धोकर उसे एक ओर सरका दिया, जिसे उसकी पत्नी यानी मेरी भाभी ले गई।
दोस्त बड़े पेसोपेश में पड़े हुए नज़र आते थे। मैंने कहा : ‘आखिर बात क्या है ? लगती है वह अंग्रेज-सी, परेशान आप हैं !’’
‘मैं न होऊंगा तो होगा और कौन ?’
‘क्यों ? आपका उससे सम्बन्ध ही क्या ?’
‘बड़े कुंवर को जाके ढूंढ़ों इस वक़्त।’
‘आखिर मतलब क्या है आपका ?’
‘बेटा किसी पेड़ के नीचे होगा और ‘चंदा-चंदा’ कहकर आहें भर रहा होगा।’
मैं हंसा। बड़ा कुंवर पन्द्रह का, चंदा होगी तेरह या चौदह की। इनके प्रेम का इलाज मेरी राय में फकत दो-दो चांटे थे।
मैंने कहा : ‘आप भी...!’
भाभी ने कहा : ‘मगर उसने तो अभी खाना भी नहीं खाया है ? दस बज रहे हैं। पूस की ठंड है। मेरी तो दांती बज रही है। जन्म लिया था सुअर ने ठाकुर के घर, घूमा है तो नटनी के पीछे। मेरी तो उसने इज़्ज़त बिगाड़ दी।’
मेरे दोस्त हठात् उठ खड़े हुए। मैं जानता था, वे ठाकुर हैं ज़रूर, पर सीधे-सादे आदमी हैं। वे दो बार कांग्रेस के अंहिसा-आन्दोलनों में जेल भी हो आए थे। बोले : ‘तो उसे ढूंढ़ ही लाऊं ?’
‘कहां जाएंगे आप ?’ मैंने कहा।
रात तब बारह गरज रही थी। दूर कहीं बघर्रे की गुर्राहट सुनायी दे रही थी, और चारों तरफ अंधकार था।
‘मुझे लालटेन नहीं, मेरी टॉर्च दे दो।’ उन्होंने कहा, और कानों पर गुलूबंद बांध लिया। मैं बड़े चक्कर में पड़ा। यह सब मेरे लिए ऐसा था जैसे किसी जासूसी उपन्यास का हिस्सा हो। मैं भी झट से तैयार हो गया।
जब भाई दरवाजे पर आए तो मैं वहां हाथ में डंडा लिए खड़ा था। भाभी की आंखें मुझे साथ जाते देखकर प्रसन्न दिखाई दीं। उनकी राय में चंदा को मार डालने में भी कोई हरज न था, क्योंकि वह उनके छोटे बेटे पर जादू कर रही थी, बड़े घर में आने के लिए। भाई साहब का मत और था। वे कहते थे कि साला आजकल की प्रेम की किताबें पढ़कर बावला हो गया है। नटनी से इश्क करके समझता है कि बड़ी तरक्की कर रहा है। बल्कि एक गरीब लड़की को फुसला रहा है। औरत में अकल होती ही कहां है ? और मैंने उनके तर्कों को सुना। मुझे मुस्कराहट भी आई। स्त्री अपने पुत्र को दोषहीन समझती है, क्योंकि वह उसके छलछिद्रों को नहीं समझती, अपनी स्त्री-जाति के मायावी रूप को जानती है और पुरुष को मूर्ख मानती है। और पुरुष अपने छलावे को जानता है, स्त्री को बेवकूफ समझता है, अतः अपने ही पुत्र को दोषी मानता है।
बाहर हवा काटे खा रही थी। दोस्त ने टॉर्च जलायी। जब हम जंगल में पहुंचे तो पुकार सुनाई दी : ‘चंदा ! ओ चंदा !’
फिर सब शांत हो गया। वहीं आगे बढ़ने पर बड़ा कुंवर नरेश लौटता दिखायी दिया। बाप और बेटे की कोई बातचीत नहीं हुई। मेरे कारण तनातनी भी नहीं हुई। घर आकर नरेश ने अनमने होकर रोटी खायी। बाजरे की घी-चुपड़ी रोटी थी। मुझसे भाभी ने कहा था : ‘स्वाद में ज़्यादा न खा जाना, पेट में गचक जाएगी।’ पर उससे कह रही थीं :‘क्यों रे ? खाता क्यों नहीं ? भूख नहीं है तुझे ?’
मैं बाहर आ गया और मैंने अपना सिगरेट का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगायी।
दूसरे दिन मैं सुबह ही उठा और आज भाई साहब के साथ खेत पर चला गया।
उनके पास पचीस बीघा खेत था, उसमें कुएं की सिंचाई थी और इस वक्त गेहूं और जौं कि फसलें झूमने के लिए तैयार हो गई थीं। पखेरू उड़ाने के लिए लड़के इधर-उधर पुकार रहे थे और पानी देने वाला जुआरा लेकर हारिया बरसात के ढांढौनों की सूखी पत्तियों के पास बैठा था। मैंने देखा, नरेश चुपचाप बैठा कुछ सोच रहा था। मैंने मन ही मन निश्चित किया कि इससे बात करूंगा। लिहाज़ा जब मेरे दोस्त चले गए तो मैं नरेश के पास जा बैठा।
मैंने कहा : ‘नरेश ! तू क्या सोचा करता है ?’
वह मेरी ओर देखने लगा। बोला कुछ नहीं।
मैंने ही कहा : ‘तू जानता है कि दुनिया के लोगों की तरह मैं भी कठोर हृदय नहीं हूं। तू मेरी रचनाएं पढ़ चुका है जिनमें मैंने जांति-पांति के बन्धनों को तोड़ने की बातें लिखी हैं। मुझसे अपने दिल की बात कह दे।
नरेश के कोमल मुख पर एक नया अवसाद घिर आया, जिसमें जीवन के नये विश्वासों का अम्बार लगा था, मानो वे जो फसलों में झूमती हुई हरी-हरी बालें थीं, कट-कटकर कनक बनकर ढेर-ढेर वसुंधरा पर मनुष्य के कल्याण-स्वप्न का प्रतीक बनकर सामने निखार लेकर उपस्थित हो गई थीं। मेरी अन्तरात्मा उस भीगे खेत-सी विभोर हो उठी। यह आयु कितनी मादक, कितनी वितृष्ण होती है, जब सारी दुनिया इसलिए फैली हुई पड़ी रहती है कि उस पर अपने ही चरणों के वैभव से चलना है। हिमगिरियों से भी ऊंचे अरमानों पर जब सूर्य अपनी देदीप्यमान किरणों को प्रतिक्षिप्त करता है तब मानो दिगंतों में नया आलोक विकीर्ण होकर अंधकार के-से भविष्य की मोटी-मोटी पर्तों को फाड़कर भीतर तक चेतना फैला जाता है। मैं जानता हूं, इसी आयु पर पुरुष के भीतर पौरुष परिपक्व होता है और उधर चंदा की ही आयु पर बालिका स्त्री बनने लगती है। मानो तितली बनकर फूलों का मधु ले-लेकर उड़ जाने के पहले, यह किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें वह कीट रेशम अपने उदर के भीतर से बुनता है और संसार के लिए उगलता है। यह वह आयु है जिसे मनुष्य की शाश्वत कोमलता, रंगीन और स्वप्निल झिलमिल ने आज तक, मनु से लेकर आज तक, अपने काव्य-भवन में प्रवेश करने के पहले, देहलीज़ बनाकर लगा दिया है। सौंदर्य अपनी नई अंगड़ाई लेकर मानो बचपन की नींद को छोड़ना चाहता है। वे अनजान मिठास-भरे दिन, जो बाल्यावस्था में होंठों पर पंखुड़ियों की भांति फिसलते हैं, इस वय पर आकर मानो रस भरी फल की फांकों-सी छाया-माया भरकर नया रूप धारण कर लेते हैं। और मैंने सोचा कि यह धरती ऐसे ही कितने-कितने युगों से मनुष्य की अमर चेतना का प्रवाह अपने भीतर अपने कण-कण में धारण करती हुई, हर भोर की बेला में नये-नये कुड़कते कान्तारों में गुंजन-भरी, डाली-डाली पर मधुर-मधुर फूल खिलाती है।
मैंने स्नेह से नरेश की ओर देखा। किन्तु उसके कपोल आरक्त थे और वह धूप से पीले-पीले जगमगाते-से अधूरे किले की ओर एकटक देख रहा था।
मैंने फिर भी कुछ नहीं पूछा। आज मौन का प्रारम्भ कल अनवरत वाणी का स्त्रोत बन जाएगा, यही मैंने मन में सोच लिया।
किंतु सांझ की बेला जब फिर घर लौटती गायों के सींगों के बीच से निकलकर नगरों पर लौटती हुई आ गई तब मैं और सुखराम धीरे-धीरे घूमते हुए जंगल की ओर चल पड़े। आज हम जिस ओर गए थे उधर झील लहरा रही थी। सांझ की पीली-पीली चादर झील पर ऐसे गिर गई थी कि मुझे वह कोई भिक्षुणी-सी दिखायी दी। सुखराम आज पहले से अधिक चिन्तित था। आज हम दोनों एक स्थान पर जाकर बैठ गए। घनी झाड़ियों में हम घिरे हुए थे, वहां कुछ छोटे-छोटे देवालय थे। उनके पीछे कोई बाग था, जिसमें अब देखभाल न होने के कारण बड़े-बड़े इमली के पेड़ थे जिनपर कौओं की कांव-कांव सुनाई दे रही थी।
अचानक हमने सुना, झाड़ी के पीछे किसी ने कहा : ‘चंदा ! तू सच कह, मेरी बात मानेगी ?’
मैंने स्वर से पहचान लिया कि यह नरेश का स्वर था।
सुखराम गम्भीर था। उसमें मुझे एक भी विचलित भाव नहीं मिला।
चंदा की आवाज आई : ‘मैं सच कहती हूँ, राजा ! मुझे लगता है, मैं इस अधूरे किले की मालकिन हूं। पर न जाने क्यों, यहां मैं इतनी दूर रहती हूं।’’
इसे सुनकर सुखराम जैसे थर्रा उठा और उसने कांपकर मेरा हाथ पकड़ लिया।
‘मैं तुझे वहां ले जा सकता हूं।’ नरेश का स्वर सुनाई दिया।
‘तुम्हें डर नहीं लगेगा ?’
‘डरूंगा क्यों ? लोग यह भी तो कहते हैं कि यहां बघेरा आता है और आज तक हम-तुम यहां आने से नहीं डरे, तो अब ही क्या डरने की बात हो सकती है !’
‘तुम सचमुच बड़े बहादुर हो।’
‘अच्छा, यह तो बता, तुझे किसने बताया कि यह किला तेरा है ?’
चंदा हंसी। कहा : ‘मैंने कल दादा के बक्स में एक तस्वीर पायी थी। वह बिलकुल मुझ-सी थी। उसे देखकर मैं कुछ भी समझ नहीं पायी। वह औरत बिलकुल मेम-सी लगती थी और उसकी तस्वीर के पीछे एक और तस्वीर छपी थी। वह किसी पुरानी ठकुरानी की तस्वीर थी। न जाने क्यों, मैंने जब से उसे देखा है, मेरे मन में चाह हो उठी है कि मैं भी वैसी बन जाऊं।’’
हठात् सुखराम का भर्राया स्वर उठा : ‘चंदा ! चंदा हो !’
और फिर लगा, झाड़ियों के पीछे कोई भागा। जब हम वहां पहुंचे, कोई नहीं था। सन्नाटा छाया हुआ था। सुखराम अत्यन्त विचलित था। मैं समझा नहीं कि आखिर बात क्या थी। सुखराम अपने-आप बुड़बुड़ाया, ‘फिर आग लगेगी, फिर धुआं उठेगा।’ और वह भयानक से अधूरे किले की ओर देखकर ठठाकर हंसा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह विकराल लग रहा था। उसने मानो अधूरे किले से कहा : ‘तू गिर कर मिट्टी में मिल जा, अभागे ! तूने इस धऱती पर रहने वालों को कभी चैन से नहीं रहने दिया।’
मैंने पुकारा : ‘सुखराम !’
‘सच कहता हूं।’ सुखराम ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर कहा :‘मैं सच कहता हूं बाबू भैया ! जिस दिन इसकी नींव खुदी थी, उस दिन इसमें नर-बलि दी गयी थी, क्योंकि तब प्रेत को चौकीदार बना देने का कायदा था। जो ज़िंदे आदमी की हड्डियों पर खड़ा किया है, वह क्या कभी आदमी को चैन दे सकता है ? इस किले में भाई-भाई का नहीं रहा। इसी के लिए भाभी ने देवर को जहर दिया। इसी किले में देवर के मरने पर देवर की गर्भ वाली बहू रातोंरात भागकर जंगल में छिपी और ठकुरानी को एक जोगी ने जंगल में जापा कराया। फिर उसे वहीं नटों में छोड़ गया, क्योंकि नटों में कोई जान का खतरा नहीं था। जब बच्चा दो बरस का हो गया तो वह ठकुरानी नाचने वाली बनकर बदला लेने आई, और अभागिन कहां तो बदला लेने आई थी, कहां खुद शिकार हो गई। जेठ नहीं जानता था, पर अपने भाई की बहू पर आशिक हो गया। ठकुरानी की चाह पूरी होने को थी, वह उसका खून कर देती, पर एक अफसोस रह गया कि वह एक दरबान की मुहब्बत में फंस गई। राजा को मालूम हुआ तो उसने ठकुरानी को हीरों की, मोतियों की लड़ों की पोशाक भेजी। ठकुरानी ने उन्हें चक्की में धरकर, पीस कर चूरा करके राजा को भेज दिया और खुद दरबान के साथ भाग निकली, पर दरबान पकड़ा गया और ठकुरानी मार डाली गई। दरबान ने कैद से छूटकर बच्चे को पाला। वह बच्चा बड़ा हुआ तो नट बना।’
‘फिर ?’ मैंने कहा।
मेरा इलाजी एक और भी आश्चर्यजनक व्यक्ति था। वह गले में मालाएं पहनता, सिर पर साफा बांधे रहता और हाथों में कांच के कड़े पहनता। वह इतने पुराने युग का था और मैं अपने को नितान्त आधुनिकता समझता था। मैं कभी इन गंवार इलाजों में भरोसा नहीं करता, पर त ही कुछ ऐसी पड़ गई कि मुझे झुकना पड़ गया। वह जंगल से रुखड़ी तोड़कर लाता, किसी को उसके बारे में नहीं बताता, पर मेरे सामने बैठकर जादू-सा करता। कभी उसमें फूंक मारता, कभी आंखें फाड़कर आसमान की तरफ देखता और कभी झूमर-सी मारता हुआ चटाचट आवाज़ करके अपनी अंगुलियां चटकाता। मैं सब समझता था कि ये सब इसके मध्यकालीन अंधविश्वास हैं। परंतु वह एक दिन इस बात पर नाराज हो गया। उसने कहा कि वह किसीके भी सामने यह रूखड़ी खोलने की बात नहीं करता, पर क्योंकि मैं शहरी हूं, इसलिए उसने इसमें कोई डर महसूस नहीं किया। उसने मुस्कराकर कहा : बाबू ! तुम बिलिया और बैंगन के पत्ते का फरक नहीं जानते, फिर तुमसे क्या डर !’
उसके स्वर में कहीं व्यंग्य था जैसा हम शहरी लोगों में गांववालों के प्रति होता है।
मैं मुस्कराया। तब उसने चिढ़कर कहा : ‘बाबू भैया ! तुम तो फिर भी अपने हो, मेरी इस रूखड़ी पर जब मन्तर डोला था तब साब अजंट थर्रा गया था।’
अब मेरे कान ज़रा खड़े हुए।
‘सो कैसे ?’ मैंने पूछा। और आज पहली बार मैंने उसके मुख की ओर देखा। साफे, मूंछों और गाय की धूल ने उसको ढंक लिया था। उसका रंग तांबे की तरह तपा हुआ था। आंखों में एक चमक थी। अब वह लगभग चालीस बरस का हो गया था। उसकी सीधी लम्बी नाक बड़ी सुन्दर थी। वह एक घुटने तक की धोती और कुछ लम्बा-सा खुले गले का कोट पहने था। और मैंने कल्पना की कि एक दिन वह सुखराम नट चौड़ी हड्डियों का गबरू जवान रहा होगा। उसकी आंखें बहुत सुन्दर रही होंगी, जिसके दोनों ओर अब गोल लकीरें खिंच गई थीं।
उस दिन वह चला गया।
सातवें दिन उसने पट्टी खोल दी और कहा : ‘आज बाबू भैया, मेरे संग घूमने चलो। तुम्हें अपनी दवाई का जादू दिखाऊँगा। ‘मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा—ज़रूर इन रूखड़ियों की वैज्ञानिक खोज होनी चाहिए। पर मुसीबत तो यह है कि वे लोग गुरु-परंपरा से पायी हुई इन चीज़ों को हवा तक नहीं देते। सदियों से जो काम हो चुका है, उसको ये लोग ईश्वरीय समझकर उसे सुलझाने के बजाय धार्मिक और दैवी बनाकर उलझाने में ही अपना गौरव समझते हैं।
आज हम लोग घूमने थोड़ी ही दूर गए। फुलवारी में बैठे रहे। उसके बीचोंबीच एक सफेद महल था। मैंने पूछा : ‘यह कब का बना है ?’
सुखराम ने कहा : ‘जब इस राजा की अमलदारी शुरू हुई थी, तब पहले राजा ने इसे बनवाया था।’
महल सुन्दर था। जाड़े की शाम। डूबते सूरज की किरणें बेरों के सुगन्धित जंगल पर पड़कर अमलतासों और सेमल के पेड़ों पर फिसल रही थी। और फिर कच्चे दगरे की गाय-भैंसों के खुरों से उठी धूल पर आर पार हो जाने का प्रयत्न कर रही थीं। चारों ओर ठंडक थी। दूर एक पेड़ के नीचे हनुमान जी थे, लाल सिन्दूर में लगे; और एक पहलवान नंगे बदन, अखाड़े की मिट्टी को मले हुए, लंगोट बांधे, दनादन बैठक लगा रहा था। एकमात्र कमरख के फलहीन पेड़ के सामने वह मुझे बड़ा अजीब-सा लग रहा था।
गांव की शाम की गंदगी, परेशानी सब धीरे-धीरे उतरते अंधेरे में छिपती चली जा रही थी और चारों ओर लौटते पक्षियों का कलरव अंधेरे के पावों के नीचे तिरता-तिरता दबा जा रहा था। मन्दिरों की झालरों और घंटो की आवाज़ अब ऐसी सुनायी देती थी जैसे किसी ने तांता जोड़ दिया हो। और दूर बजती बैलों की घंटियां और भी एक सूनापन भर-भर देती थीं।
सुखराम ने कहा : ‘कल और आगे चलेंगे।’
मैंने कहा : ‘वह क्या है ?’
सुखराम ने कहा : ‘रोज तो देखते ही हो।’
मैंने कहा : ‘किला है। किसने बनवाया था ?’
सुखराम ने उत्तर दिया :‘उसी राजा के बेटे ने।’
मैंने कहा : ‘छोटा ही है।’
‘रह गया है।’
मैंने पूछा :‘क्या मतलब ?’
‘‘अधूरा किला है।’
‘शायद राजा मर गया था ?’
‘हां, बाबू भैया। कहते हैं, राज्य के लिए उसकी भाभी ने उसे ज़हर दे दिया था। वह जानते हुए पी गया था।’
कहते हुए सुखराम की आंखों में पानी छलक आया। मैं समझा नहीं। मैंने कहा : ‘ऐसा क्यों हुआ सुखराम ? और इससे तुम्हें रोने की क्या त है ?’
वह आंसू पोंछकर मुस्कराया। उसने कहा : ‘कुछ नहीं बाबू भैया ! अब जमाना बदल गया है। राजाओं के ही राज चले गए तो इन बातों से फायदा ही क्या है !’
‘नहीं, नहीं सुखराम’, मेरे भिखारी उपन्यासकार ने याचना की, ‘बताओ न ! मैं तो परदेसी हूं। उस दिन तुम साहब के थर्राने की बात कहते-कहते रुक गए थे, आज तुम इस बात को भी छिपा रहे हो।’
परन्तु वह कुछ नहीं बोला। उसने बात बदलकर कहा : ‘क्यों, अब चल सकते हो न ?’
‘क्यों नहीं। कल और भी चलेंगे।’
‘हां, अब क्या डर है ?’
‘सुखराम, वह क्या है ?’ मैंने एक ओर हाथ उठाकर कहा।
वह एक नीला पहाड़ था। उसपर एक गहरा सन्नाटा था। लगता था, आसमान से उतरता अंधेरा पहले वहां इकट्ठा हो गया है और अब हवा के झोंके उसीसे उड़ा-उड़ाकर उसे इधर-उधर फैला रहे हैं। सुखराम ने कहा : ‘चलो बाबू भैया ! चलो।’
उसने जैसे मेरी बांसुरी में से तरह-तरह के राग निकलते देखकर किसी भी राग को पकड़ने की जगह बांसुरी के रंध्र को ही उंगली से दबाकर बन्द कर दिया। मेरी सारी जिज्ञासा रुंधी हुई पड़ी रह गई।
तीसरे दिन जब हम लोग जंगल में पहुंचे तो सामने धुंआ उठता हुआ दिखायी दिया। मैंने कहा : ‘यह क्या है ?’
‘यह हमारी बस्ती है।’ सुखराम ने कहा।
मैंने देखा, छोटे-छोटे घर थे। और अब सांझ उस जंगल से बस्ती को चारों ओर से घिराव डालकर दबाए ले रही थी। शायद ही दस घर हों। मैंने सोचा—यह संसार कितनी तरह का है ? कहीं बम्बई की भीड़, कहीं आदमी ऐसे भी सन्नाटे में रहकर उम्र गुज़ार देता है ? सामने एक बड़ा-सा कुआं था। मैं उसकी ओर बढ़ा, पर वहां पहुंच कर ठिठक गया। एक बच्ची, लगभग तेरह या चौदह वर्ष की, वहां पानी खींच रही थी; वह ऊंचा घाघरा और फरिया पहने थी। फरिया इस वक़्त उसके कंधों के नीचे पड़ी थी। उसकी ओर मैंने देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ। उसके नेत्र नीले, बाल सुनहले और रंग भभूका सफेद था। उसकी नाक कुछ आगे उठी हुई थी और उसके गालों पर सुर्खी थी। वह मुस्करायी।
‘कौन ?’ सुखराम ने कहा : ‘चन्दा, अभी घर नहीं गई ?’
‘रोटी बनाकर धर आई हूं दादा (पिता), पानी का एक डोल लेने आई थी।’
मुझे अब मालूम हुआ कि वह सुखराम की बेटी थी। परन्तु कितना अजीब था। वह लड़की बिलकुल अंग्रेज मालूम देती थी। उसकी आवाज़ में कितना तीखा पतलापन था कि मेरा विश्वास विचलित हो उठा।
सुखराम ने बीड़ी सुलगा ली और फिर ध्यान में डूब गया। मैं सोच नहीं सका। सामने पहाड़ के पैरों पर चांदी की बेड़ी-सी एक इमारत खड़ी थी। मैंने उसकी ओर इशारा करके पूछा : ‘सुखराम, वह क्या है ?’
लड़की ने हंसकर कहा :‘डाक बंगला। पहले यहां सा’ब लोग आया करते थे। अब तो उनका राज ही चला गया।’
वह फिर हंसी और सुखराम की आंखों में एक छाया-सी डबडबा आई, कातर, परन्तु अर्निद्य, सुखावह नहीं, अपने-आप में पूर्ण।
उस दिन और बात नहीं हुई। मैं घर आ गया। जिनके घर ठहरा था, वे मित्र खाने के समय यह बताने में लगे रहे कि अब वे नई जिन्दगी शुरू करना चाहते थे। उनका दिल गांव से ऊब गया था। बड़ी देर तक वे गांव की निंदा करते रहे, परंतु उन्होंने सारांश यही निकाला कि गांव हर हालत में शहर से अच्छा होता है, अतः वे यहीं रहेंगे। मेरे पांव की बात चली। फिर सुखराम की बात आई। मैंने उसकी लड़की के बारे में भी ज़िक्र किया। मेरे दोस्त ने हुक्का पास सरकाया और खाने की थाली में हाथ धोकर उसे एक ओर सरका दिया, जिसे उसकी पत्नी यानी मेरी भाभी ले गई।
दोस्त बड़े पेसोपेश में पड़े हुए नज़र आते थे। मैंने कहा : ‘आखिर बात क्या है ? लगती है वह अंग्रेज-सी, परेशान आप हैं !’’
‘मैं न होऊंगा तो होगा और कौन ?’
‘क्यों ? आपका उससे सम्बन्ध ही क्या ?’
‘बड़े कुंवर को जाके ढूंढ़ों इस वक़्त।’
‘आखिर मतलब क्या है आपका ?’
‘बेटा किसी पेड़ के नीचे होगा और ‘चंदा-चंदा’ कहकर आहें भर रहा होगा।’
मैं हंसा। बड़ा कुंवर पन्द्रह का, चंदा होगी तेरह या चौदह की। इनके प्रेम का इलाज मेरी राय में फकत दो-दो चांटे थे।
मैंने कहा : ‘आप भी...!’
भाभी ने कहा : ‘मगर उसने तो अभी खाना भी नहीं खाया है ? दस बज रहे हैं। पूस की ठंड है। मेरी तो दांती बज रही है। जन्म लिया था सुअर ने ठाकुर के घर, घूमा है तो नटनी के पीछे। मेरी तो उसने इज़्ज़त बिगाड़ दी।’
मेरे दोस्त हठात् उठ खड़े हुए। मैं जानता था, वे ठाकुर हैं ज़रूर, पर सीधे-सादे आदमी हैं। वे दो बार कांग्रेस के अंहिसा-आन्दोलनों में जेल भी हो आए थे। बोले : ‘तो उसे ढूंढ़ ही लाऊं ?’
‘कहां जाएंगे आप ?’ मैंने कहा।
रात तब बारह गरज रही थी। दूर कहीं बघर्रे की गुर्राहट सुनायी दे रही थी, और चारों तरफ अंधकार था।
‘मुझे लालटेन नहीं, मेरी टॉर्च दे दो।’ उन्होंने कहा, और कानों पर गुलूबंद बांध लिया। मैं बड़े चक्कर में पड़ा। यह सब मेरे लिए ऐसा था जैसे किसी जासूसी उपन्यास का हिस्सा हो। मैं भी झट से तैयार हो गया।
जब भाई दरवाजे पर आए तो मैं वहां हाथ में डंडा लिए खड़ा था। भाभी की आंखें मुझे साथ जाते देखकर प्रसन्न दिखाई दीं। उनकी राय में चंदा को मार डालने में भी कोई हरज न था, क्योंकि वह उनके छोटे बेटे पर जादू कर रही थी, बड़े घर में आने के लिए। भाई साहब का मत और था। वे कहते थे कि साला आजकल की प्रेम की किताबें पढ़कर बावला हो गया है। नटनी से इश्क करके समझता है कि बड़ी तरक्की कर रहा है। बल्कि एक गरीब लड़की को फुसला रहा है। औरत में अकल होती ही कहां है ? और मैंने उनके तर्कों को सुना। मुझे मुस्कराहट भी आई। स्त्री अपने पुत्र को दोषहीन समझती है, क्योंकि वह उसके छलछिद्रों को नहीं समझती, अपनी स्त्री-जाति के मायावी रूप को जानती है और पुरुष को मूर्ख मानती है। और पुरुष अपने छलावे को जानता है, स्त्री को बेवकूफ समझता है, अतः अपने ही पुत्र को दोषी मानता है।
बाहर हवा काटे खा रही थी। दोस्त ने टॉर्च जलायी। जब हम जंगल में पहुंचे तो पुकार सुनाई दी : ‘चंदा ! ओ चंदा !’
फिर सब शांत हो गया। वहीं आगे बढ़ने पर बड़ा कुंवर नरेश लौटता दिखायी दिया। बाप और बेटे की कोई बातचीत नहीं हुई। मेरे कारण तनातनी भी नहीं हुई। घर आकर नरेश ने अनमने होकर रोटी खायी। बाजरे की घी-चुपड़ी रोटी थी। मुझसे भाभी ने कहा था : ‘स्वाद में ज़्यादा न खा जाना, पेट में गचक जाएगी।’ पर उससे कह रही थीं :‘क्यों रे ? खाता क्यों नहीं ? भूख नहीं है तुझे ?’
मैं बाहर आ गया और मैंने अपना सिगरेट का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगायी।
दूसरे दिन मैं सुबह ही उठा और आज भाई साहब के साथ खेत पर चला गया।
उनके पास पचीस बीघा खेत था, उसमें कुएं की सिंचाई थी और इस वक्त गेहूं और जौं कि फसलें झूमने के लिए तैयार हो गई थीं। पखेरू उड़ाने के लिए लड़के इधर-उधर पुकार रहे थे और पानी देने वाला जुआरा लेकर हारिया बरसात के ढांढौनों की सूखी पत्तियों के पास बैठा था। मैंने देखा, नरेश चुपचाप बैठा कुछ सोच रहा था। मैंने मन ही मन निश्चित किया कि इससे बात करूंगा। लिहाज़ा जब मेरे दोस्त चले गए तो मैं नरेश के पास जा बैठा।
मैंने कहा : ‘नरेश ! तू क्या सोचा करता है ?’
वह मेरी ओर देखने लगा। बोला कुछ नहीं।
मैंने ही कहा : ‘तू जानता है कि दुनिया के लोगों की तरह मैं भी कठोर हृदय नहीं हूं। तू मेरी रचनाएं पढ़ चुका है जिनमें मैंने जांति-पांति के बन्धनों को तोड़ने की बातें लिखी हैं। मुझसे अपने दिल की बात कह दे।
नरेश के कोमल मुख पर एक नया अवसाद घिर आया, जिसमें जीवन के नये विश्वासों का अम्बार लगा था, मानो वे जो फसलों में झूमती हुई हरी-हरी बालें थीं, कट-कटकर कनक बनकर ढेर-ढेर वसुंधरा पर मनुष्य के कल्याण-स्वप्न का प्रतीक बनकर सामने निखार लेकर उपस्थित हो गई थीं। मेरी अन्तरात्मा उस भीगे खेत-सी विभोर हो उठी। यह आयु कितनी मादक, कितनी वितृष्ण होती है, जब सारी दुनिया इसलिए फैली हुई पड़ी रहती है कि उस पर अपने ही चरणों के वैभव से चलना है। हिमगिरियों से भी ऊंचे अरमानों पर जब सूर्य अपनी देदीप्यमान किरणों को प्रतिक्षिप्त करता है तब मानो दिगंतों में नया आलोक विकीर्ण होकर अंधकार के-से भविष्य की मोटी-मोटी पर्तों को फाड़कर भीतर तक चेतना फैला जाता है। मैं जानता हूं, इसी आयु पर पुरुष के भीतर पौरुष परिपक्व होता है और उधर चंदा की ही आयु पर बालिका स्त्री बनने लगती है। मानो तितली बनकर फूलों का मधु ले-लेकर उड़ जाने के पहले, यह किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें वह कीट रेशम अपने उदर के भीतर से बुनता है और संसार के लिए उगलता है। यह वह आयु है जिसे मनुष्य की शाश्वत कोमलता, रंगीन और स्वप्निल झिलमिल ने आज तक, मनु से लेकर आज तक, अपने काव्य-भवन में प्रवेश करने के पहले, देहलीज़ बनाकर लगा दिया है। सौंदर्य अपनी नई अंगड़ाई लेकर मानो बचपन की नींद को छोड़ना चाहता है। वे अनजान मिठास-भरे दिन, जो बाल्यावस्था में होंठों पर पंखुड़ियों की भांति फिसलते हैं, इस वय पर आकर मानो रस भरी फल की फांकों-सी छाया-माया भरकर नया रूप धारण कर लेते हैं। और मैंने सोचा कि यह धरती ऐसे ही कितने-कितने युगों से मनुष्य की अमर चेतना का प्रवाह अपने भीतर अपने कण-कण में धारण करती हुई, हर भोर की बेला में नये-नये कुड़कते कान्तारों में गुंजन-भरी, डाली-डाली पर मधुर-मधुर फूल खिलाती है।
मैंने स्नेह से नरेश की ओर देखा। किन्तु उसके कपोल आरक्त थे और वह धूप से पीले-पीले जगमगाते-से अधूरे किले की ओर एकटक देख रहा था।
मैंने फिर भी कुछ नहीं पूछा। आज मौन का प्रारम्भ कल अनवरत वाणी का स्त्रोत बन जाएगा, यही मैंने मन में सोच लिया।
किंतु सांझ की बेला जब फिर घर लौटती गायों के सींगों के बीच से निकलकर नगरों पर लौटती हुई आ गई तब मैं और सुखराम धीरे-धीरे घूमते हुए जंगल की ओर चल पड़े। आज हम जिस ओर गए थे उधर झील लहरा रही थी। सांझ की पीली-पीली चादर झील पर ऐसे गिर गई थी कि मुझे वह कोई भिक्षुणी-सी दिखायी दी। सुखराम आज पहले से अधिक चिन्तित था। आज हम दोनों एक स्थान पर जाकर बैठ गए। घनी झाड़ियों में हम घिरे हुए थे, वहां कुछ छोटे-छोटे देवालय थे। उनके पीछे कोई बाग था, जिसमें अब देखभाल न होने के कारण बड़े-बड़े इमली के पेड़ थे जिनपर कौओं की कांव-कांव सुनाई दे रही थी।
अचानक हमने सुना, झाड़ी के पीछे किसी ने कहा : ‘चंदा ! तू सच कह, मेरी बात मानेगी ?’
मैंने स्वर से पहचान लिया कि यह नरेश का स्वर था।
सुखराम गम्भीर था। उसमें मुझे एक भी विचलित भाव नहीं मिला।
चंदा की आवाज आई : ‘मैं सच कहती हूँ, राजा ! मुझे लगता है, मैं इस अधूरे किले की मालकिन हूं। पर न जाने क्यों, यहां मैं इतनी दूर रहती हूं।’’
इसे सुनकर सुखराम जैसे थर्रा उठा और उसने कांपकर मेरा हाथ पकड़ लिया।
‘मैं तुझे वहां ले जा सकता हूं।’ नरेश का स्वर सुनाई दिया।
‘तुम्हें डर नहीं लगेगा ?’
‘डरूंगा क्यों ? लोग यह भी तो कहते हैं कि यहां बघेरा आता है और आज तक हम-तुम यहां आने से नहीं डरे, तो अब ही क्या डरने की बात हो सकती है !’
‘तुम सचमुच बड़े बहादुर हो।’
‘अच्छा, यह तो बता, तुझे किसने बताया कि यह किला तेरा है ?’
चंदा हंसी। कहा : ‘मैंने कल दादा के बक्स में एक तस्वीर पायी थी। वह बिलकुल मुझ-सी थी। उसे देखकर मैं कुछ भी समझ नहीं पायी। वह औरत बिलकुल मेम-सी लगती थी और उसकी तस्वीर के पीछे एक और तस्वीर छपी थी। वह किसी पुरानी ठकुरानी की तस्वीर थी। न जाने क्यों, मैंने जब से उसे देखा है, मेरे मन में चाह हो उठी है कि मैं भी वैसी बन जाऊं।’’
हठात् सुखराम का भर्राया स्वर उठा : ‘चंदा ! चंदा हो !’
और फिर लगा, झाड़ियों के पीछे कोई भागा। जब हम वहां पहुंचे, कोई नहीं था। सन्नाटा छाया हुआ था। सुखराम अत्यन्त विचलित था। मैं समझा नहीं कि आखिर बात क्या थी। सुखराम अपने-आप बुड़बुड़ाया, ‘फिर आग लगेगी, फिर धुआं उठेगा।’ और वह भयानक से अधूरे किले की ओर देखकर ठठाकर हंसा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह विकराल लग रहा था। उसने मानो अधूरे किले से कहा : ‘तू गिर कर मिट्टी में मिल जा, अभागे ! तूने इस धऱती पर रहने वालों को कभी चैन से नहीं रहने दिया।’
मैंने पुकारा : ‘सुखराम !’
‘सच कहता हूं।’ सुखराम ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर कहा :‘मैं सच कहता हूं बाबू भैया ! जिस दिन इसकी नींव खुदी थी, उस दिन इसमें नर-बलि दी गयी थी, क्योंकि तब प्रेत को चौकीदार बना देने का कायदा था। जो ज़िंदे आदमी की हड्डियों पर खड़ा किया है, वह क्या कभी आदमी को चैन दे सकता है ? इस किले में भाई-भाई का नहीं रहा। इसी के लिए भाभी ने देवर को जहर दिया। इसी किले में देवर के मरने पर देवर की गर्भ वाली बहू रातोंरात भागकर जंगल में छिपी और ठकुरानी को एक जोगी ने जंगल में जापा कराया। फिर उसे वहीं नटों में छोड़ गया, क्योंकि नटों में कोई जान का खतरा नहीं था। जब बच्चा दो बरस का हो गया तो वह ठकुरानी नाचने वाली बनकर बदला लेने आई, और अभागिन कहां तो बदला लेने आई थी, कहां खुद शिकार हो गई। जेठ नहीं जानता था, पर अपने भाई की बहू पर आशिक हो गया। ठकुरानी की चाह पूरी होने को थी, वह उसका खून कर देती, पर एक अफसोस रह गया कि वह एक दरबान की मुहब्बत में फंस गई। राजा को मालूम हुआ तो उसने ठकुरानी को हीरों की, मोतियों की लड़ों की पोशाक भेजी। ठकुरानी ने उन्हें चक्की में धरकर, पीस कर चूरा करके राजा को भेज दिया और खुद दरबान के साथ भाग निकली, पर दरबान पकड़ा गया और ठकुरानी मार डाली गई। दरबान ने कैद से छूटकर बच्चे को पाला। वह बच्चा बड़ा हुआ तो नट बना।’
‘फिर ?’ मैंने कहा।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book