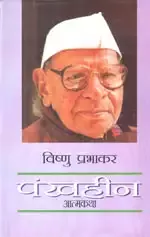|
जीवनी/आत्मकथा >> पंखहीन पंखहीनविष्णु प्रभाकर
|
411 पाठक हैं |
||||||
विष्णु प्रभाकर का जीवन परिचय..
Pankhheen
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
मूर्धन्य साहित्यकार विष्णु प्रभाकर की यह आत्मकथा उनके अपने जीवन का वृतान्त होने के साथ-साथ बीसवीं शताब्दी के आरंभ से देश और उसके समाज में चले सामाजिक राजनीतिक आन्दोलनों का, तथा इन सबके साथ साहित्य की विविध गतिविधियों का, चारों ओर नजर डालता आईना है। समूची पिछली सदी को अपने में समेटता यह जीवन-वृत्त एक प्रकार से उस युग का गहराई से किया गया चित्रण तथा विश्लेषक लेखा-जोखा है जिसमें देश और उसके जन ने एक बिलकुल नया, आधुनिक, निर्माणशील जीवन जीना आरंभ किया है।
पिछले 75 वर्षों से लगातार लिख रहे विष्णु प्रभाकर का लेखन उस समय आरंभ हुआ जब हिन्दी साहित्य आरंभिक तैयारियों के बाद विषय, भाषा, अभिव्यक्ति आदि सभी दृष्टियों से प्रौढ़ता प्राप्त करने लगा था। साहित्य विधाओं में एक के बाद एक, छायावाद प्रगतिवाद प्रयोगवाद नई कहानी इत्यादि युग बन और मिट रहे थे, परंतु नई उक्कीसवीं शताब्दी के इन आरंभिक वर्षों में जो सब प्रायः समाप्त हो चुका है। उन्होंने यह समाप्त उत्थान पतन राजधानी दिल्ली में रहकर स्वयं अपनी आँखों से देखा और उसमें भाग लिया है। इसे सौभाग्य ही कहा जाना चाहिए। कि नब्बे वर्ष की सुदीर्घ आयु पार करके वे आज भी हमारे बीच हैं। और शताब्दी के इस घटनाचक्र तथा इतिहास को लिपिबद्ध किया है।
यह आत्मकथा विष्णु प्रभाकर के अपने जीवन के उतार-चढ़ाव के साथ-साथ भारतीय समाज के ऐतिहासिक परिवर्तन का भी रोमांचक दस्तावेज़ है।
यशस्वी साहित्यकार विष्णुप्रभाकर की बहुप्रतीक्षित आत्मकथा...साथ ही पूरी एक सदी के साहित्यिक जीवन तथा समाज और देश का चारों ओर दृष्टि डालता आईना और दस्तावेज़।
पिछले 75 वर्षों से लगातार लिख रहे विष्णु प्रभाकर का लेखन उस समय आरंभ हुआ जब हिन्दी साहित्य आरंभिक तैयारियों के बाद विषय, भाषा, अभिव्यक्ति आदि सभी दृष्टियों से प्रौढ़ता प्राप्त करने लगा था। साहित्य विधाओं में एक के बाद एक, छायावाद प्रगतिवाद प्रयोगवाद नई कहानी इत्यादि युग बन और मिट रहे थे, परंतु नई उक्कीसवीं शताब्दी के इन आरंभिक वर्षों में जो सब प्रायः समाप्त हो चुका है। उन्होंने यह समाप्त उत्थान पतन राजधानी दिल्ली में रहकर स्वयं अपनी आँखों से देखा और उसमें भाग लिया है। इसे सौभाग्य ही कहा जाना चाहिए। कि नब्बे वर्ष की सुदीर्घ आयु पार करके वे आज भी हमारे बीच हैं। और शताब्दी के इस घटनाचक्र तथा इतिहास को लिपिबद्ध किया है।
यह आत्मकथा विष्णु प्रभाकर के अपने जीवन के उतार-चढ़ाव के साथ-साथ भारतीय समाज के ऐतिहासिक परिवर्तन का भी रोमांचक दस्तावेज़ है।
यशस्वी साहित्यकार विष्णुप्रभाकर की बहुप्रतीक्षित आत्मकथा...साथ ही पूरी एक सदी के साहित्यिक जीवन तथा समाज और देश का चारों ओर दृष्टि डालता आईना और दस्तावेज़।
यह आत्मकथा : दिशाहीन सफ़र
काल और दिक् असीम और अनन्त हैं। आयु की सीमा में बँधा मनुष्य उनकी थाह नहीं ले सकता, फिर भी काल की सीमा का अतिक्रमण करके वह भूत और भविष्य में सदा झाँकता आया है। उसका अपना एक आनन्द होता है। उसमें जो भी विगत हो चुका है उसका फिर से जीना अधिक चुनौती-भरा होता है। आगत की कल्पना में हम स्वतन्त्र होते हैं, पर जो विगत है वहाँ तो हम बँधे हैं उससे जो घट चुका है। यही बंधन एक चुनौती है और चुनौती हमेशा आनन्द को गहराती है, उसे दृष्टि-सम्पन्न बनाती है और मूल्यों से जोड़ती है। काल के सन्दर्भ में होने वाला हर परिवर्तन मूल्यों का परिवर्तन है।
और फिर विगत की परिणति तो वर्तमान के ‘मैं’ में होती है। ‘मैं’ से महत्त्वपूर्ण हैं वे स्थितियाँ जो उसका निर्माण करती हैं। उन्हीं स्थितियों और उन स्थितियों से जुड़े व्यक्तियों का वर्णन करना चाहते हैं हम। मेरे लिए आत्मकथा लिखने का दावा मात्र दम्भ होगा क्योंकि उसमें न तो कुछ ऐसा है जो युग के सन्दर्भ में महत्त्वपूर्ण है, न मुझमें इतना साहस है कि अपने को, अपने से ही मुक्त करके देख सकूँ, अपने चारों ओर घिर आए संसार को।
एक और दृष्टि है अपने अतीत में झाँकने की। व्यक्ति की पड़ताल तो आलोचक और समीक्षक दोनों करते हैं पर उनकी दृष्टि तीसरे व्यक्ति की होती है। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं अपनी पड़ताल करता है तो उसके सामने कोई और नहीं होता, वह स्वयं ही होता है। इस प्रक्रिया में उसे अपनी जड़ों की ओर लौटना बहुत आवश्यक है। मैं आज जो भी हूँ, वह कैसे सम्भव हुआ, किन प्रक्रियाओं में से गुजरने के बाद मैं इस मंजि़ल पर पहुँचा, इसकी जाँच-पड़ताल करना बहुत कठिन नहीं है तो, बहुत आसान भी नहीं है। कठिन और आसान–ये दोनों शब्द सापेक्ष हैं, विशेषकर लेखक के सम्बन्ध में।
मैं स्वीकार करूँगा कि मैं भी एक लेखक हूँ, न सही महान, अकिंचन ही सही, पर लेखक अवश्य हूँ। आप उसे मेरा दम्भ ही समझ सकते हैं लेकिन यह सच है मैं नहीं जानता वह कौन-सा ‘मैं’ है जो लेखक होने की प्रक्रिया में से गुज़रता है क्योंकि जब वह लिखने की प्रक्रिया में से गुजर रहा होता है तब वह वहाँ होता है, जहाँ से उसे स्वयं उसकी खबर नहीं मिलती। देखने में लेखक भी दूसरे व्यक्तियों की तरह साधारण व्यक्ति होता है। लेकिन किसी-किसी व्यक्ति में अवश्य ऐसा कुछ होता है जो उसे औरों से अलग करता है हीरे को तराशा जा सकता है पर उसकी चमक अपनी होती है। वही चमक लेखक को साधारण जन से अलग करती है, अर्थात इसी चमक के कारण ही वह अपनी पहचान अलग बनाता है। साधारण जन अनुभव के देश को सह कर ही रह जाता है पर लेखक उसी को रचना का रूप देकर सार्वजनिक कर देता है।
यह सार्वजनिक बनाना लेखक को एक ऐसे संसार में ले जाता है जहाँ हर किसी के लिए पहुँचना सम्भव नहीं। मैं आज अपने आपको उसी संसार में ले जाना चाहता हूँ और आपको भी आमन्त्रित करता हूँ सहयात्री होने के लिए। जहाँ से मुझे मेरी याद है, वहाँ धुँधला-धुँधला अवश्य है पर मेरे अनुभव संसार का मूल स्रोत वही है। अतीत में झाँकना बहुत अच्छा लगता है पर उसको परखने की अपनी दृष्टि होती है। अतीत हमेशा समृद्ध होता है, समृद्धि का अर्थ मात्र ऐश्वर्य और वैभव नहीं बल्कि दुःख, पीड़ा, वेदना और दर्द भी है, बल्कि वही अधिक है। ओस की बूँद निश्चय ही पुलक से भरती है लेकिन किसी की आँख का आँसू उसे दर्द से भर देता है और इसी दर्द को सहने की यातना में से गुजरे बिना कोई सृजक या लेखक नहीं बन सकता। खोज का यह विकट मार्ग ही सृजक की नियति है।
तो इस भूमिका के साथ कहानी का आरम्भ करूँ-एक दिशाहीन सफर की तलाश में उस सत्य की जो अजाना है और अजाना ही रहेगा। फि़राक़ गोरखपुरी ने किसी और सन्दर्भ में फरमाया है यह शेर पर, यह मेरी तलाश के लिए उतना ही सत्य है :
और फिर विगत की परिणति तो वर्तमान के ‘मैं’ में होती है। ‘मैं’ से महत्त्वपूर्ण हैं वे स्थितियाँ जो उसका निर्माण करती हैं। उन्हीं स्थितियों और उन स्थितियों से जुड़े व्यक्तियों का वर्णन करना चाहते हैं हम। मेरे लिए आत्मकथा लिखने का दावा मात्र दम्भ होगा क्योंकि उसमें न तो कुछ ऐसा है जो युग के सन्दर्भ में महत्त्वपूर्ण है, न मुझमें इतना साहस है कि अपने को, अपने से ही मुक्त करके देख सकूँ, अपने चारों ओर घिर आए संसार को।
एक और दृष्टि है अपने अतीत में झाँकने की। व्यक्ति की पड़ताल तो आलोचक और समीक्षक दोनों करते हैं पर उनकी दृष्टि तीसरे व्यक्ति की होती है। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं अपनी पड़ताल करता है तो उसके सामने कोई और नहीं होता, वह स्वयं ही होता है। इस प्रक्रिया में उसे अपनी जड़ों की ओर लौटना बहुत आवश्यक है। मैं आज जो भी हूँ, वह कैसे सम्भव हुआ, किन प्रक्रियाओं में से गुजरने के बाद मैं इस मंजि़ल पर पहुँचा, इसकी जाँच-पड़ताल करना बहुत कठिन नहीं है तो, बहुत आसान भी नहीं है। कठिन और आसान–ये दोनों शब्द सापेक्ष हैं, विशेषकर लेखक के सम्बन्ध में।
मैं स्वीकार करूँगा कि मैं भी एक लेखक हूँ, न सही महान, अकिंचन ही सही, पर लेखक अवश्य हूँ। आप उसे मेरा दम्भ ही समझ सकते हैं लेकिन यह सच है मैं नहीं जानता वह कौन-सा ‘मैं’ है जो लेखक होने की प्रक्रिया में से गुज़रता है क्योंकि जब वह लिखने की प्रक्रिया में से गुजर रहा होता है तब वह वहाँ होता है, जहाँ से उसे स्वयं उसकी खबर नहीं मिलती। देखने में लेखक भी दूसरे व्यक्तियों की तरह साधारण व्यक्ति होता है। लेकिन किसी-किसी व्यक्ति में अवश्य ऐसा कुछ होता है जो उसे औरों से अलग करता है हीरे को तराशा जा सकता है पर उसकी चमक अपनी होती है। वही चमक लेखक को साधारण जन से अलग करती है, अर्थात इसी चमक के कारण ही वह अपनी पहचान अलग बनाता है। साधारण जन अनुभव के देश को सह कर ही रह जाता है पर लेखक उसी को रचना का रूप देकर सार्वजनिक कर देता है।
यह सार्वजनिक बनाना लेखक को एक ऐसे संसार में ले जाता है जहाँ हर किसी के लिए पहुँचना सम्भव नहीं। मैं आज अपने आपको उसी संसार में ले जाना चाहता हूँ और आपको भी आमन्त्रित करता हूँ सहयात्री होने के लिए। जहाँ से मुझे मेरी याद है, वहाँ धुँधला-धुँधला अवश्य है पर मेरे अनुभव संसार का मूल स्रोत वही है। अतीत में झाँकना बहुत अच्छा लगता है पर उसको परखने की अपनी दृष्टि होती है। अतीत हमेशा समृद्ध होता है, समृद्धि का अर्थ मात्र ऐश्वर्य और वैभव नहीं बल्कि दुःख, पीड़ा, वेदना और दर्द भी है, बल्कि वही अधिक है। ओस की बूँद निश्चय ही पुलक से भरती है लेकिन किसी की आँख का आँसू उसे दर्द से भर देता है और इसी दर्द को सहने की यातना में से गुजरे बिना कोई सृजक या लेखक नहीं बन सकता। खोज का यह विकट मार्ग ही सृजक की नियति है।
तो इस भूमिका के साथ कहानी का आरम्भ करूँ-एक दिशाहीन सफर की तलाश में उस सत्य की जो अजाना है और अजाना ही रहेगा। फि़राक़ गोरखपुरी ने किसी और सन्दर्भ में फरमाया है यह शेर पर, यह मेरी तलाश के लिए उतना ही सत्य है :
न मंज़िल है, न मंज़िल का पता है,
मुहब्बत बस रास्ता ही रास्ता है।
मुहब्बत बस रास्ता ही रास्ता है।
इस सत्य की तलाश में कोई मंज़िल नहीं होती, इसलिए वैज्ञानिक सत्य से बढ़कर सत्य की तलाश को महत्त्व देते हैं।
तो इसी तलाश की प्रक्रिया के साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ अपने अतीत से। अतीत से जुडना इसलिए आवश्यक है कि वहीं तो मेरी चेतना के अंकुर फूटे थे। ये अंकुर जीवन के अन्तिम क्षण तक मुझे अपने अस्तित्व का बोध कराते रहेंगे। जुड़ने की इस प्रक्रिया में जैसा हमने पहले कहा कि अपनी जड़ों की तलाश बहुत आवश्यक है।
जड़ अर्थात बृहत्तर कुटुम्ब, जाति और समाज। इनसे अपने सम्बन्धों की विवेचना करना बहुत आसान नहीं क्योंकि जिस जाति से मेरा सम्बन्ध माना जाता है, उसका अपना इतिहास सर्वसम्मत नहीं है। फिर भी जो सुलभ है उसी के आधार पर अपनी जड़ों की तलाश हम निश्चय ही करेंगे। उसका भी अपना एक आनन्द है, वह आनन्द जो अनिवार्यता से जुड़ा है। उस भूमिका के साथ संक्षेप में इतना कहना पर्याप्त होगा कि मैं सुप्रसिद्र अग्रवाल जाति की एक शाखा ‘राजवंश अग्रवाल’ से सम्बन्ध रखता हूँ।
राजवंश अग्रवाल जाति का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। अन्तिम मुगलों के समय में इसका जन्म हुआ था। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन इससे पूर्व अग्रवाल जाति के इतिहास की खोज भी करना चाहेंगे। अग्रवाल जाति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है और इसके आदि पुरुष कौन थे इस सम्बन्ध में बहुत मतभेद हैं। वैसे आजकल इस जाति के इतिहासकारों का यह मानना है कि इसका इतिहास बहुत पुराना है, जो पौराणिक काल तक जाता है।
लेकिन राजा अग्रसेन से पहले राजाओं का प्रामाणिक इतिहास न मिलने के कारण हमने यह मान लिया है कि राजा अग्रसेन ही वर्तमान अग्रवाल जाति के आदि पुरुष थे। उनके परिवार और वंश के बारे में भी बहुत मतभेद है लेकिन अन्नतः अधिकतर लोग इस बात पर सहमत हो गए हैं कि उनकी साढ़े तेरह रानियाँ थीं। ‘आधी’ की कोई सर्वसम्मत व्याख्या नहीं है। लेकिन मैंने बचपन में सुना था कि उनकी एक रानी राजकन्या नहीं थी, इसलिए उन्हें आधी रानी कहा गया। उन सब रानियों से राजा अग्रसेन को दो-दो पुत्रों और एक-एक पुत्री की प्राप्ति हुई और उसी समय गोत्रों का भी निर्णय हुआ। साढ़े तेरह रानियों के आधार पर साढ़े तेरह गोत्र निश्चित हुए।
राजा अग्रसेन क्षत्रिय थे, लेकिन अग्रवाल जाति वैश्य मानी जाती है। अब वह कैसे क्षत्रिय से वैश्य हुए, इस बारे में भी बहुत सी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। उनमें एक किंवदंती यह भी है कि त्रेता युग में जब परशुराम जी, राजा जनक के यहाँ सीता स्वयंवर में टूटे हुए धनुष की खबर पाकर क्रोध में भरे वहाँ जा रहे थे
तो रास्ते में उन्हें अग्रसेन जी शिकार पर जाते हुए मिल गए। अपने ध्यान में उन्होंने परशुराम जी को नहीं देखा, न उन्होंने प्रणाम किया जिसके कारण परशुराम जी क्रोधित हुए और अग्रेसन जी को निःसंतान होने का श्राप दे दिया। श्राप से अग्रसेन जी बहुत दुःखी होकर महर्षि विश्वामित्र के आश्रम गए और उनसे सलाह माँगी। विश्वामित्र जी ने उनको क्षत्रिय
धर्मत्यागकर वैश्य धर्म अपनाने की सलाह दी, साथ ही क्षत्रियों का चिह्न राजछत्र, चँवर आदि भी धारण करने को कहा।
यहाँ यह प्रश्न उठता है कि महाराजा अग्रसेन का वास्तविक काल क्या था। इस सम्बन्ध में भी बहुत मतभेद है लेकिन डॉ. स्वराज्य मणि अग्रवाल अपनी पुस्तक ‘अग्रसेन, अग्रोहा, अग्रवाल’ में यह मानती हैं कि ‘वह निश्चय ही कलियुग के प्रारंभिक युग में हुए। उनका काल सर्व सहमति से यह माना जा सकता है।’ आगे वह अनेक विद्वानों की चर्चा करती हुई लिखती हैं-वास्तव में उनका काल महालक्ष्मी व्रत कथा के अनुसार कलि सम्वत् के प्रारम्भ से 108 वर्ष के भीतर ही माना जाना चाहिए जो आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व का होता है।
लेकिन हमारा प्रयोजन राजा अग्रसेन के काल का निर्णय करना नहीं है। इतना कहना पर्याप्त होगा कि अग्रवाल जाति बहुत प्राचीन है। लेकिन इतिहास में सिकन्दर और अग्रगण की जो चर्चा आती है, वह इस दृष्टि से सही नहीं ठहरती। उसको सही प्रमाणित करना हमारा उद्देश्य भी नहीं है। हम तो यहाँ केवल यही कहना चाहते हैं कि अग्रवाल जाति का इतिहास बहुत पुराना है, कम से कम पाँच हज़ार साल पुराना। पारजीटर के अनुसार यही काल राम का भी है। ऊपर हमने जो परशुराम जी की उनसे भेंट की चर्चा की है, वह इस बात को प्रमाणित करती है।
तब यह मान्यता कि सिकन्दर ने जिन गणों को पराजित किया उनमें एक गण अग्रगण था और उसी ने वहाँ के पराजित होने के बाद वर्तमान अग्रोहा के पास अपनी नई बस्ती बसाई, सही नहीं ठहरती। यहाँ हम इस उलझन में नहीं पड़ना चाहते। यही मान लेते हैं कि अग्रवाल जाति का इतिहास बहुत पुराना है और वर्तमान अग्रोहा से उनका सम्बन्ध भी उतना ही पुराना है।
इसी अग्रवाल जाति का सम्बन्ध राजवंशी अग्रवालों से है। राजवंश अग्रवाल शब्द को लेकर भी बहुत मतभेद है। लेकिन इस मतभेद को सुलझाने के लिए मैं पहले अपने वंश की कहानी, जितनी मैं जान सका, उतनी बताना चाहूँगा। मेरे पास ग्यारह पीढ़ियों का वंश-वृक्ष है। मेरे पुरखे कहाँ से आए पता नहीं। मेरी याद में वह हमारे कस्बे में ‘मवाने वाले’ के नाम से जाने जाते थे। कब कौन सा पुरखा मवाना से आकर वर्तमान कस्बे मीरापुर में बस गया था, उसका भी किसी के पास सही
ब्योरा नहीं मिलता। मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ था तब हमारा खानदान ‘हकलों का खानदान’ कहलाता था। अपनी-अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए ऐसे ‘उपनाम’ कस्बे में सभी खानदानों के साथ जुड़ गए थे और ये उपनाम उनकी किसी न किसी विशेषता को रेखांकित करते थे।
सुना था कि मुझसे सात पीढ़ी पहले के मेरे एक पुरखा लाला मंगूशाह से लेकर मेरी पीढ़ी तक कोई न कोई व्यक्ति हकला होता रहा है। यह रोग संक्रामक नहीं है और न पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है फिर भी हीन भाव का द्योतक यह रूप न जाने कैसे मेरी अगली पीढ़ी तक अपने अस्तित्व का बोध कराता रहा।
भारत के उत्तर में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन प्रान्त है, उत्तर प्रदेश। इतने धर्म, इतनी जातियाँ, इतनी भाषाएँ और इतनी संस्कृतियाँ मिलेंगी इस प्रान्त में कि इसका कोई नाम ही नहीं रह गया। सबको अपने में समोकर यह दिशासूचक बनकर रह गया है लेकिन वर्तमान युग में इस प्रान्त को भाषा के अनुसार बाँटने की बात बराबर उठती रही है और उसके परिणाम स्वरूप अभी एक नए प्रान्त का इसी के गर्भ से जन्म हुआ है। उसका नाम है ‘उत्तरांचल’ और वह उसके उत्तर में जो कुमायूँ और गढ़वाल दो पहाड़ी प्रदेश हैं, उनको मिलाकर बनाया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण कुमायूँ प्रदेश बहुत
प्रसिद्ध है और उतना ही प्रसिद्ध है गढ़वाल प्रदेश धार्मिक तीर्थों के लिए। अलकनन्दा, भागीरथी, जाह्ववी, मंदाकिनी, नंदाकिनी, विष्णु गंगा, धौली गंगा, नारद गंगा और पाताल गंगा....अन्त नहीं इन नाना-रूप धाराओं का, पर सबको अपने में समेटती हुई भागीरथी जब अलकनन्दा से मिलने देवप्रयाग में आती है, तब वह बस एक ही धारा बन जाती है और उस धारा का नाम हो जाता है गंगा। नाम-हीन धारा को ‘गंगा’ अर्थात् नदी ही कह सकते हैं। जैसे गंगा का अर्थ है नदी वैसे ही उत्तर प्रदेश का अर्थ है वह प्रदेश जो, देश के ‘उत्तर’ में है लेकिन अब तो वहाँ ‘उत्तरांचल’ राज्य की स्थापना हो गई है।
फिर भी वहाँ से बहकर आने वाली गंगा नदी अन्ततः उत्तर प्रदेश में ही आती है। अब भी उत्तर प्रदेश में बहुत-सी जातियाँ वर्ण और वर्ग हैं। जब ये जातियाँ वर्ग और वर्ण अपने-अपने नाम से अतीत हो रहते हैं, तभी उनका नाम ‘मनुष्य’ सार्थक होता है। मेरे जन्म के समय का उत्तर प्रदेश बँट गया, लेकिन ‘मनुष्य’ नहीं बँटा है। भले ही प्रान्तों में अलग-अलग जातियाँ रहती हैं पर अन्ततः वह मनुष्य ही हैं। इस दृष्टि से न केवल प्रान्त और देश बल्कि सारा विश्व मनुष्यों का वास है।
मेरे देश का नाम भारत है और मेरा प्रदेश बँट जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश कहलाता है। हाँ, उत्तराखण्ड में शिव-पार्वती की क्रीड़ा भूमि और गंगा आदि सरिताओं की जन्मभूमि, नगाधिराज हिमालय जो पृथ्वी का मानदण्ड है और है भारत की संस्कृति, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक, ये सब अब उत्तर प्रदेश में नहीं रहे हैं, पर उसके उत्तर में तो हैं ही।
दक्षिण भाग में है रणबांकुरे और मिठबोले बुंदेलों का बुंदेलखण्ड। जितना शौर्य उतना ही माधुर्य। बुंदेलखण्डी भाषा जैसी मीठी भाषा विश्व में दुर्लभ है।
यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अयोध्या है तो आर्य और द्रविड़ों के समन्वय के प्रतीक शिव के त्रिशूल पर ठहरी, काशी है और वह सारनाथ भी है जहाँ तथागत बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था।
शाहजहाँ से पूर्व मुग़लों की राजधानी आगरा और फतहपुर सीकरी भी यहीं पर है। इसी आगरा में स्थित है विश्व का सातवाँ आश्चर्य और शाश्वत प्रेम का प्रतीक ताजमहल।
उत्तराखण्ड के अलग हो जाने पर भी विभिन्न धर्मों के नाना तीर्थों से पटा पड़ा है यह प्रदेश। पश्चिमी भू- खण्ड में लीला-पुरुषोत्तम कृष्ण की ब्रज भूमि है। यहीं पर मय दानव द्वारा निर्मित मेरठ है जहाँ दासता के विरुद्ध पहले संगठित विद्रोह ने जन्म लिया था। इसी का एक नाम मय-राष्ट्र भी है। कहते हैं कि कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर के लिए राजधानी के रूप में मय दानव ने इस नगर का निर्माण किया था।
निश्चय ही वह उस युग में स्थापत्य कला का श्रेष्ठ विशेषज्ञ रहा होगा। इसी पश्चिमी भूखण्ड में मेरठ के पास एक जिला है मुज़फ्फ़रनगर। इसकी पश्चिमी सीमा यमुना है तो पूर्वी सीमा गंगा। इसी भूखण्ड में राष्ट्रभाषा हिन्दी का जन्म हुआ। यहाँ की बोलचाल की भाषा ‘कौरवी’ कहलाती है। हिन्दी का मूल प्राकृत रूप यही है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस सम्बन्ध में बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।
यहीं पर गंगा-तट के पास हस्तिनापुर से दूर एक छोटा सा कस्बा है मीरापुर। इसी कस्बे में रोजी-रोटी की तलाश में आकर बसा होगा मेरा कोई पुरखा। वह वैश्य वर्ण की अग्रवाल शाखा में सिंघल गोत्रिय था। उसके आने के बाद या आने से पहले मूल अग्रवालों में से एक और शाखा फूट निकली थी। यह अठारहवीं सदी के आरम्भ अर्थात् सन् 1707 की बातें हैं। इस शाखा के फूटने की कहानी बहुत रोमांचक है।
सन् 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की शक्ति निरन्तर क्षीण होती चली गई। उसके बेटे बहादुरशाह का राज्य मार्च सन् 1712 तक ही चल पाया। उसके बाद राजदरबार और राजमहल षड्यंत्रों के अड्डे बन गए। बहादुरशाह के चार बेटे थे। अपने तीन भाइयों का कत्ल करके जहाँदारशाह गद्दी पर बैठने में सफल हुआ लेकिन वह ग्यारह महीने ही राज्य कर सका। उसके बड़े भाई के बेटे फर्रु़खसियर ने विद्रोह कर दिया और अन्त में उसने जहाँदारशाह को मारकर गद्दी हथिया ली।
इस अभियान में उसके प्रबल समर्थक थे सैयद बंधु, इसलिए यह स्वाभाविक था कि उनका दबदबा बढ़ जाता। एक समय तो ऐसा आया कि वे जिसे चाहते उसे गद्दी पर बैठा देते और जिसे चाहते गद्दी से उतार देते थे। इसलिए में वे ‘किंगमेकर’ के नाम से प्रसिद्ध हैं। बड़े सैयद अब्दुल्ला खान और छोटे हुसैन अली खान दोनों मेरे कस्बे मीरापुर से पाँच मील दूर तहसील जानसठ के रहने वाले थे। उनके अत्यन्त विश्वसनीय साथी थे मीरापुर- निवासी लाल रतन चन्द। मेरे पुरखों की कहानी इन्हीं लाला रतन चन्द से जुड़ी है।
लाल रतन चन्द्र का जन्म सुप्रसिद्ध अग्रवाल जाति में सन् 1665 में हुआ था। इनके पिता लाला जयलाल सिंह गोयल आढ़त के बड़े व्यापारी थे। रतन चन्द पिता के साथ काम करते थे। वह बहुत कुशाग्रबुद्धि और हिसाब किताब में माहिर थे। उनकी यह ख्याति सुनकर सैयद बंधुओं ने उन्हें अपना खज़ांची नियुक्त कर लिया। धीरे-धीरे वह उनसे इतने हिल मिल गए कि अग्रवाल जाति के नेता उन्हें शक की दृष्टि से देखने लगे।
अग्रवाल जाति के सम्बन्ध में हम पहले लिख आए हैं। वे लोग उस समय के अनुसार खान-पान के मामले में बड़े कट्टर थे। मुसलमान के हाथ का छुआ भी वह नहीं खाते थे। सैयद बंधुओं के साथ रहने के कारण लाला रतन चन्द खान-पान के सम्बन्ध में उतने कट्टर नहीं रह गए थे। जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें एक दिन अग्रवालों की मूल शाखा से अलग हो जाना पड़ा। इस सम्बन्ध में भी कोई सर्वसम्मत राय नहीं है। एक प्रवाद यह प्रचलित है
कि राजा रतन चन्द ने सैयद बंधुओं के साथ एक दस्तरखान पर बैठकर खाना खा लिया था। इसी अपराध के द्ण्डस्वरूप अग्रवाल जाति के नेताओं ने उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया। जिन लोगों ने जाति बहिष्कृत होने का खतरा उठाकर उनका साथ दिया वे ही पहले ‘राजा की बिरादरी’ फिर ‘राजा शाही’ और अन्त में ‘राजवंशी’ के रूप में जाने गए।
एक कथा और प्रचलित है कि इस अवधि में उनके बड़े बेटे का विवाह निश्चित हुआ। निमंत्रण पत्र के रूप में उस समय ऐसे अवसरों पर गिदौड़ (गुड़ या खांड के लड्डू) बाँटे जाते थे। राजा रतन चन्द ने भी ऐसा ही किया और यह घोषणा की कि जो व्यक्ति इन लड्डुओं को स्वीकार करेंगे वह मेरे अनुयायी और समर्थक माने जाएँगे। अधिकांश अग्रवालों ने इन लड्डुओं को स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने किया वे राजा की बिरादरी या ‘राजाशाही’ कहलाने लगे। कालान्तर में उन्होंने अपने को राजवंशी अग्रवाल कहना शुरू कर दिया और आज तक इसी नाम से जाने जाते हैं। उस समय वे केवल जिला मेरठ, सहारनपुर, मुज़फ़्फ़रनगर, और बिजनौर तक ही सीमित थे लेकिन बाद में आसपास के ज़िलों और राजस्थान में भी फैल गए।
लेकिन राजा रतन चन्द के मूल अग्रवालों से अलग होने पर सहमति नहीं है। अनेक इतिहासकारों ने अलग-अलग मत प्रकट किए हैं।
इस सम्बन्ध में डॉ. स्वराज्य मणि अग्रवाल ने अपनी खोजपूर्ण पुस्तक में लिखा है, ‘आज अग्रवालों के समस्त भेदों के नाम देखते हुए ‘राजवंशी वणिक’ भेद ही एक ऐसा भेद लगता है जो ‘राजक्षतृन्यान्वय वणिक’ के अर्थ से साम्य रखता है। अतः हो सकता है कि ये राजवंशी अग्रवाल के नाम से प्रसिद्ध हुए हों। डॉ. परमेश्वरी लाल गुप्त का अनुमान है। कि हो सकता है राजा की बिरादरी राजाशाही या राजवंशी अग्रवाल आरम्भ में एक ही रहे हों। बाद में जब राजा रतन चन्द के समय में बिरादरी के पृथकत्व की बात आई तो राजा रतनचन्द के समर्थक राजा की बिरादरी के नाम से विकसित हुए होंगे और राजवंशी वणिक ‘राजक्षतृन्यान्वय वणिक’ की मूल शाखा से विकसित हुए होंगे।2
राजवंशी शब्द को लेकर बहुत मतभेद है लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि यह शब्द सन् 1901 से पहले से प्रचलित था।
यहाँ हम इस शब्द को लेकर विवाद में नहीं पड़ना चाहते। इस सम्बन्ध में श्री निहालचन्द जी ने अपनी पुस्तक ‘वैश्य-अग्रवाल राजवंश समाज का इतिहास’ में पृष्ठ 40 पर जो लिखा है वह हम स्वीकार करते हैं। उनके शब्द हैं, ‘उपरोक्त समस्त उल्लेखों और तथ्यों का गहराई से अध्ययन करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि राजवंश अग्रवाल समाज उसी परम्परा से जुड़ा है, जिसमें कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन ने राजकन्याओं और नागकन्याओं की सन्तानों को उनकी
अलग-अलग पहचान के लिए राजवंशी और नागवंशी संस्तरणों में रखा था। तब से यह लोग इन्हीं नामों से अंकित होते आए हैं। अठारहवीं शताब्दी में राजवंशियों में एक प्रतापी वीर पुरुष राजा रतनचंद के नाम से हुए जिन्होंने मुगल दरबार में उच्च पद प्राप्त किया और उस काल में अत्यन्त प्रभावशाली एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कट्टरपंथी एवं रुढ़िवादी लोगों के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके साथ परिवारों और व्यक्तियों के समूह जुड़ते चले गए और इस प्रकार
-----------------------------------
1. डॉ. स्वराज्य मणिअग्रवाल-‘अग्रसेन, अग्रवाल, अग्राहा’, पृष्ठ 180
2. ‘वैश्य-अग्रवाल राजवंश समाज का इतिहास’ पृष्ठ-38
जिन लोगों ने उनका साथ दिया वे ‘राजा की बिरादरी’ और ‘राजाशाही’ के नाम से अंकित हुए और आगे चल कर उन्होंने अपना पुराना नाम ‘राजवंशी’ ही धारण कर लिया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि राजा रतनचंद्र एक ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, जिन्होंने राजवंश अग्रवाल समाज को गौरवान्वित किया, किन्तु जो समाज उनसे पहले से ही चला आ रहा था, उसका उन्हें प्रवर्तक बताना तो अतिशयोक्ति ही होगी क्योंकि राजवंशी अग्रवाल के आदि पुरुष या प्रवर्तक तो राजा अग्रसेन ही हैं।
अन्तिम मुगलों के इतिहास मुगलों के इतिहास में सैयद बंधुओं और राजा रतनचंद का क्या रोल रहा है और कितना प्रभाव था उनका, इसको लेकर हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेन्द्र वर्मा ने एक बहुत सुन्दर नाटक लिखा है, ‘छोटे सैयद बड़े सैयद।’ इस नाटक को पढ़ते हुए और देखते हुए हम सही रूप में राजा रतनचंद की योग्यता और शक्ति से परिचित हो सकते हैं। सैयद बंधुओं की सफलता के पीछे राजा रतनचंद का ही मस्तिष्क था। वह न होते तो सैयद बंधु आपस में लड़कर मर जाते। समय-समय पर उन्होंने कैसे दोनों भाइयों के बिगड़ते सम्बन्धों को सुधारा और राजनीति की कैसी-कैसी
विलक्षण चालें चलीं, यह सब नाटक को पढ़कर ही जाना जा सकता है। वे शासन प्रणाली में भी बहुत कुशल थे लेकिन सैयद बंधुओं का जो स्वप्न था वह पूरा नहीं हुआ और षड्यंत्र करने वाले खुद ही राजदरबार के षड्यन्त्रों में उलझ गए। अन्त में मोहम्मद शाह ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। छोटे सैयद की पहले ही हत्या हो चुकी थी। अन्तिम युद्ध में अब्दुल्ला और रतनचंद की फौजें भी हार गईं और उनके साथी सब गिरफ्तार कर लिए गए। उन सब बंदियों को सज़ा देते हुए मोहम्मद शाह की दृष्टि सबसे पहले राजा रतनचंद पर पड़ती है। वह पूछते हैं, ‘राजा रतनचंद, आपको अपने बारे में कुछ कहना है।
तो इसी तलाश की प्रक्रिया के साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ अपने अतीत से। अतीत से जुडना इसलिए आवश्यक है कि वहीं तो मेरी चेतना के अंकुर फूटे थे। ये अंकुर जीवन के अन्तिम क्षण तक मुझे अपने अस्तित्व का बोध कराते रहेंगे। जुड़ने की इस प्रक्रिया में जैसा हमने पहले कहा कि अपनी जड़ों की तलाश बहुत आवश्यक है।
जड़ अर्थात बृहत्तर कुटुम्ब, जाति और समाज। इनसे अपने सम्बन्धों की विवेचना करना बहुत आसान नहीं क्योंकि जिस जाति से मेरा सम्बन्ध माना जाता है, उसका अपना इतिहास सर्वसम्मत नहीं है। फिर भी जो सुलभ है उसी के आधार पर अपनी जड़ों की तलाश हम निश्चय ही करेंगे। उसका भी अपना एक आनन्द है, वह आनन्द जो अनिवार्यता से जुड़ा है। उस भूमिका के साथ संक्षेप में इतना कहना पर्याप्त होगा कि मैं सुप्रसिद्र अग्रवाल जाति की एक शाखा ‘राजवंश अग्रवाल’ से सम्बन्ध रखता हूँ।
राजवंश अग्रवाल जाति का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। अन्तिम मुगलों के समय में इसका जन्म हुआ था। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन इससे पूर्व अग्रवाल जाति के इतिहास की खोज भी करना चाहेंगे। अग्रवाल जाति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है और इसके आदि पुरुष कौन थे इस सम्बन्ध में बहुत मतभेद हैं। वैसे आजकल इस जाति के इतिहासकारों का यह मानना है कि इसका इतिहास बहुत पुराना है, जो पौराणिक काल तक जाता है।
लेकिन राजा अग्रसेन से पहले राजाओं का प्रामाणिक इतिहास न मिलने के कारण हमने यह मान लिया है कि राजा अग्रसेन ही वर्तमान अग्रवाल जाति के आदि पुरुष थे। उनके परिवार और वंश के बारे में भी बहुत मतभेद है लेकिन अन्नतः अधिकतर लोग इस बात पर सहमत हो गए हैं कि उनकी साढ़े तेरह रानियाँ थीं। ‘आधी’ की कोई सर्वसम्मत व्याख्या नहीं है। लेकिन मैंने बचपन में सुना था कि उनकी एक रानी राजकन्या नहीं थी, इसलिए उन्हें आधी रानी कहा गया। उन सब रानियों से राजा अग्रसेन को दो-दो पुत्रों और एक-एक पुत्री की प्राप्ति हुई और उसी समय गोत्रों का भी निर्णय हुआ। साढ़े तेरह रानियों के आधार पर साढ़े तेरह गोत्र निश्चित हुए।
राजा अग्रसेन क्षत्रिय थे, लेकिन अग्रवाल जाति वैश्य मानी जाती है। अब वह कैसे क्षत्रिय से वैश्य हुए, इस बारे में भी बहुत सी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। उनमें एक किंवदंती यह भी है कि त्रेता युग में जब परशुराम जी, राजा जनक के यहाँ सीता स्वयंवर में टूटे हुए धनुष की खबर पाकर क्रोध में भरे वहाँ जा रहे थे
तो रास्ते में उन्हें अग्रसेन जी शिकार पर जाते हुए मिल गए। अपने ध्यान में उन्होंने परशुराम जी को नहीं देखा, न उन्होंने प्रणाम किया जिसके कारण परशुराम जी क्रोधित हुए और अग्रेसन जी को निःसंतान होने का श्राप दे दिया। श्राप से अग्रसेन जी बहुत दुःखी होकर महर्षि विश्वामित्र के आश्रम गए और उनसे सलाह माँगी। विश्वामित्र जी ने उनको क्षत्रिय
धर्मत्यागकर वैश्य धर्म अपनाने की सलाह दी, साथ ही क्षत्रियों का चिह्न राजछत्र, चँवर आदि भी धारण करने को कहा।
यहाँ यह प्रश्न उठता है कि महाराजा अग्रसेन का वास्तविक काल क्या था। इस सम्बन्ध में भी बहुत मतभेद है लेकिन डॉ. स्वराज्य मणि अग्रवाल अपनी पुस्तक ‘अग्रसेन, अग्रोहा, अग्रवाल’ में यह मानती हैं कि ‘वह निश्चय ही कलियुग के प्रारंभिक युग में हुए। उनका काल सर्व सहमति से यह माना जा सकता है।’ आगे वह अनेक विद्वानों की चर्चा करती हुई लिखती हैं-वास्तव में उनका काल महालक्ष्मी व्रत कथा के अनुसार कलि सम्वत् के प्रारम्भ से 108 वर्ष के भीतर ही माना जाना चाहिए जो आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व का होता है।
लेकिन हमारा प्रयोजन राजा अग्रसेन के काल का निर्णय करना नहीं है। इतना कहना पर्याप्त होगा कि अग्रवाल जाति बहुत प्राचीन है। लेकिन इतिहास में सिकन्दर और अग्रगण की जो चर्चा आती है, वह इस दृष्टि से सही नहीं ठहरती। उसको सही प्रमाणित करना हमारा उद्देश्य भी नहीं है। हम तो यहाँ केवल यही कहना चाहते हैं कि अग्रवाल जाति का इतिहास बहुत पुराना है, कम से कम पाँच हज़ार साल पुराना। पारजीटर के अनुसार यही काल राम का भी है। ऊपर हमने जो परशुराम जी की उनसे भेंट की चर्चा की है, वह इस बात को प्रमाणित करती है।
तब यह मान्यता कि सिकन्दर ने जिन गणों को पराजित किया उनमें एक गण अग्रगण था और उसी ने वहाँ के पराजित होने के बाद वर्तमान अग्रोहा के पास अपनी नई बस्ती बसाई, सही नहीं ठहरती। यहाँ हम इस उलझन में नहीं पड़ना चाहते। यही मान लेते हैं कि अग्रवाल जाति का इतिहास बहुत पुराना है और वर्तमान अग्रोहा से उनका सम्बन्ध भी उतना ही पुराना है।
इसी अग्रवाल जाति का सम्बन्ध राजवंशी अग्रवालों से है। राजवंश अग्रवाल शब्द को लेकर भी बहुत मतभेद है। लेकिन इस मतभेद को सुलझाने के लिए मैं पहले अपने वंश की कहानी, जितनी मैं जान सका, उतनी बताना चाहूँगा। मेरे पास ग्यारह पीढ़ियों का वंश-वृक्ष है। मेरे पुरखे कहाँ से आए पता नहीं। मेरी याद में वह हमारे कस्बे में ‘मवाने वाले’ के नाम से जाने जाते थे। कब कौन सा पुरखा मवाना से आकर वर्तमान कस्बे मीरापुर में बस गया था, उसका भी किसी के पास सही
ब्योरा नहीं मिलता। मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ था तब हमारा खानदान ‘हकलों का खानदान’ कहलाता था। अपनी-अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए ऐसे ‘उपनाम’ कस्बे में सभी खानदानों के साथ जुड़ गए थे और ये उपनाम उनकी किसी न किसी विशेषता को रेखांकित करते थे।
सुना था कि मुझसे सात पीढ़ी पहले के मेरे एक पुरखा लाला मंगूशाह से लेकर मेरी पीढ़ी तक कोई न कोई व्यक्ति हकला होता रहा है। यह रोग संक्रामक नहीं है और न पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है फिर भी हीन भाव का द्योतक यह रूप न जाने कैसे मेरी अगली पीढ़ी तक अपने अस्तित्व का बोध कराता रहा।
भारत के उत्तर में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन प्रान्त है, उत्तर प्रदेश। इतने धर्म, इतनी जातियाँ, इतनी भाषाएँ और इतनी संस्कृतियाँ मिलेंगी इस प्रान्त में कि इसका कोई नाम ही नहीं रह गया। सबको अपने में समोकर यह दिशासूचक बनकर रह गया है लेकिन वर्तमान युग में इस प्रान्त को भाषा के अनुसार बाँटने की बात बराबर उठती रही है और उसके परिणाम स्वरूप अभी एक नए प्रान्त का इसी के गर्भ से जन्म हुआ है। उसका नाम है ‘उत्तरांचल’ और वह उसके उत्तर में जो कुमायूँ और गढ़वाल दो पहाड़ी प्रदेश हैं, उनको मिलाकर बनाया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण कुमायूँ प्रदेश बहुत
प्रसिद्ध है और उतना ही प्रसिद्ध है गढ़वाल प्रदेश धार्मिक तीर्थों के लिए। अलकनन्दा, भागीरथी, जाह्ववी, मंदाकिनी, नंदाकिनी, विष्णु गंगा, धौली गंगा, नारद गंगा और पाताल गंगा....अन्त नहीं इन नाना-रूप धाराओं का, पर सबको अपने में समेटती हुई भागीरथी जब अलकनन्दा से मिलने देवप्रयाग में आती है, तब वह बस एक ही धारा बन जाती है और उस धारा का नाम हो जाता है गंगा। नाम-हीन धारा को ‘गंगा’ अर्थात् नदी ही कह सकते हैं। जैसे गंगा का अर्थ है नदी वैसे ही उत्तर प्रदेश का अर्थ है वह प्रदेश जो, देश के ‘उत्तर’ में है लेकिन अब तो वहाँ ‘उत्तरांचल’ राज्य की स्थापना हो गई है।
फिर भी वहाँ से बहकर आने वाली गंगा नदी अन्ततः उत्तर प्रदेश में ही आती है। अब भी उत्तर प्रदेश में बहुत-सी जातियाँ वर्ण और वर्ग हैं। जब ये जातियाँ वर्ग और वर्ण अपने-अपने नाम से अतीत हो रहते हैं, तभी उनका नाम ‘मनुष्य’ सार्थक होता है। मेरे जन्म के समय का उत्तर प्रदेश बँट गया, लेकिन ‘मनुष्य’ नहीं बँटा है। भले ही प्रान्तों में अलग-अलग जातियाँ रहती हैं पर अन्ततः वह मनुष्य ही हैं। इस दृष्टि से न केवल प्रान्त और देश बल्कि सारा विश्व मनुष्यों का वास है।
मेरे देश का नाम भारत है और मेरा प्रदेश बँट जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश कहलाता है। हाँ, उत्तराखण्ड में शिव-पार्वती की क्रीड़ा भूमि और गंगा आदि सरिताओं की जन्मभूमि, नगाधिराज हिमालय जो पृथ्वी का मानदण्ड है और है भारत की संस्कृति, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक, ये सब अब उत्तर प्रदेश में नहीं रहे हैं, पर उसके उत्तर में तो हैं ही।
दक्षिण भाग में है रणबांकुरे और मिठबोले बुंदेलों का बुंदेलखण्ड। जितना शौर्य उतना ही माधुर्य। बुंदेलखण्डी भाषा जैसी मीठी भाषा विश्व में दुर्लभ है।
यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अयोध्या है तो आर्य और द्रविड़ों के समन्वय के प्रतीक शिव के त्रिशूल पर ठहरी, काशी है और वह सारनाथ भी है जहाँ तथागत बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था।
शाहजहाँ से पूर्व मुग़लों की राजधानी आगरा और फतहपुर सीकरी भी यहीं पर है। इसी आगरा में स्थित है विश्व का सातवाँ आश्चर्य और शाश्वत प्रेम का प्रतीक ताजमहल।
उत्तराखण्ड के अलग हो जाने पर भी विभिन्न धर्मों के नाना तीर्थों से पटा पड़ा है यह प्रदेश। पश्चिमी भू- खण्ड में लीला-पुरुषोत्तम कृष्ण की ब्रज भूमि है। यहीं पर मय दानव द्वारा निर्मित मेरठ है जहाँ दासता के विरुद्ध पहले संगठित विद्रोह ने जन्म लिया था। इसी का एक नाम मय-राष्ट्र भी है। कहते हैं कि कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर के लिए राजधानी के रूप में मय दानव ने इस नगर का निर्माण किया था।
निश्चय ही वह उस युग में स्थापत्य कला का श्रेष्ठ विशेषज्ञ रहा होगा। इसी पश्चिमी भूखण्ड में मेरठ के पास एक जिला है मुज़फ्फ़रनगर। इसकी पश्चिमी सीमा यमुना है तो पूर्वी सीमा गंगा। इसी भूखण्ड में राष्ट्रभाषा हिन्दी का जन्म हुआ। यहाँ की बोलचाल की भाषा ‘कौरवी’ कहलाती है। हिन्दी का मूल प्राकृत रूप यही है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस सम्बन्ध में बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।
यहीं पर गंगा-तट के पास हस्तिनापुर से दूर एक छोटा सा कस्बा है मीरापुर। इसी कस्बे में रोजी-रोटी की तलाश में आकर बसा होगा मेरा कोई पुरखा। वह वैश्य वर्ण की अग्रवाल शाखा में सिंघल गोत्रिय था। उसके आने के बाद या आने से पहले मूल अग्रवालों में से एक और शाखा फूट निकली थी। यह अठारहवीं सदी के आरम्भ अर्थात् सन् 1707 की बातें हैं। इस शाखा के फूटने की कहानी बहुत रोमांचक है।
सन् 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की शक्ति निरन्तर क्षीण होती चली गई। उसके बेटे बहादुरशाह का राज्य मार्च सन् 1712 तक ही चल पाया। उसके बाद राजदरबार और राजमहल षड्यंत्रों के अड्डे बन गए। बहादुरशाह के चार बेटे थे। अपने तीन भाइयों का कत्ल करके जहाँदारशाह गद्दी पर बैठने में सफल हुआ लेकिन वह ग्यारह महीने ही राज्य कर सका। उसके बड़े भाई के बेटे फर्रु़खसियर ने विद्रोह कर दिया और अन्त में उसने जहाँदारशाह को मारकर गद्दी हथिया ली।
इस अभियान में उसके प्रबल समर्थक थे सैयद बंधु, इसलिए यह स्वाभाविक था कि उनका दबदबा बढ़ जाता। एक समय तो ऐसा आया कि वे जिसे चाहते उसे गद्दी पर बैठा देते और जिसे चाहते गद्दी से उतार देते थे। इसलिए में वे ‘किंगमेकर’ के नाम से प्रसिद्ध हैं। बड़े सैयद अब्दुल्ला खान और छोटे हुसैन अली खान दोनों मेरे कस्बे मीरापुर से पाँच मील दूर तहसील जानसठ के रहने वाले थे। उनके अत्यन्त विश्वसनीय साथी थे मीरापुर- निवासी लाल रतन चन्द। मेरे पुरखों की कहानी इन्हीं लाला रतन चन्द से जुड़ी है।
लाल रतन चन्द्र का जन्म सुप्रसिद्ध अग्रवाल जाति में सन् 1665 में हुआ था। इनके पिता लाला जयलाल सिंह गोयल आढ़त के बड़े व्यापारी थे। रतन चन्द पिता के साथ काम करते थे। वह बहुत कुशाग्रबुद्धि और हिसाब किताब में माहिर थे। उनकी यह ख्याति सुनकर सैयद बंधुओं ने उन्हें अपना खज़ांची नियुक्त कर लिया। धीरे-धीरे वह उनसे इतने हिल मिल गए कि अग्रवाल जाति के नेता उन्हें शक की दृष्टि से देखने लगे।
अग्रवाल जाति के सम्बन्ध में हम पहले लिख आए हैं। वे लोग उस समय के अनुसार खान-पान के मामले में बड़े कट्टर थे। मुसलमान के हाथ का छुआ भी वह नहीं खाते थे। सैयद बंधुओं के साथ रहने के कारण लाला रतन चन्द खान-पान के सम्बन्ध में उतने कट्टर नहीं रह गए थे। जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें एक दिन अग्रवालों की मूल शाखा से अलग हो जाना पड़ा। इस सम्बन्ध में भी कोई सर्वसम्मत राय नहीं है। एक प्रवाद यह प्रचलित है
कि राजा रतन चन्द ने सैयद बंधुओं के साथ एक दस्तरखान पर बैठकर खाना खा लिया था। इसी अपराध के द्ण्डस्वरूप अग्रवाल जाति के नेताओं ने उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया। जिन लोगों ने जाति बहिष्कृत होने का खतरा उठाकर उनका साथ दिया वे ही पहले ‘राजा की बिरादरी’ फिर ‘राजा शाही’ और अन्त में ‘राजवंशी’ के रूप में जाने गए।
एक कथा और प्रचलित है कि इस अवधि में उनके बड़े बेटे का विवाह निश्चित हुआ। निमंत्रण पत्र के रूप में उस समय ऐसे अवसरों पर गिदौड़ (गुड़ या खांड के लड्डू) बाँटे जाते थे। राजा रतन चन्द ने भी ऐसा ही किया और यह घोषणा की कि जो व्यक्ति इन लड्डुओं को स्वीकार करेंगे वह मेरे अनुयायी और समर्थक माने जाएँगे। अधिकांश अग्रवालों ने इन लड्डुओं को स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने किया वे राजा की बिरादरी या ‘राजाशाही’ कहलाने लगे। कालान्तर में उन्होंने अपने को राजवंशी अग्रवाल कहना शुरू कर दिया और आज तक इसी नाम से जाने जाते हैं। उस समय वे केवल जिला मेरठ, सहारनपुर, मुज़फ़्फ़रनगर, और बिजनौर तक ही सीमित थे लेकिन बाद में आसपास के ज़िलों और राजस्थान में भी फैल गए।
लेकिन राजा रतन चन्द के मूल अग्रवालों से अलग होने पर सहमति नहीं है। अनेक इतिहासकारों ने अलग-अलग मत प्रकट किए हैं।
इस सम्बन्ध में डॉ. स्वराज्य मणि अग्रवाल ने अपनी खोजपूर्ण पुस्तक में लिखा है, ‘आज अग्रवालों के समस्त भेदों के नाम देखते हुए ‘राजवंशी वणिक’ भेद ही एक ऐसा भेद लगता है जो ‘राजक्षतृन्यान्वय वणिक’ के अर्थ से साम्य रखता है। अतः हो सकता है कि ये राजवंशी अग्रवाल के नाम से प्रसिद्ध हुए हों। डॉ. परमेश्वरी लाल गुप्त का अनुमान है। कि हो सकता है राजा की बिरादरी राजाशाही या राजवंशी अग्रवाल आरम्भ में एक ही रहे हों। बाद में जब राजा रतन चन्द के समय में बिरादरी के पृथकत्व की बात आई तो राजा रतनचन्द के समर्थक राजा की बिरादरी के नाम से विकसित हुए होंगे और राजवंशी वणिक ‘राजक्षतृन्यान्वय वणिक’ की मूल शाखा से विकसित हुए होंगे।2
राजवंशी शब्द को लेकर बहुत मतभेद है लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि यह शब्द सन् 1901 से पहले से प्रचलित था।
यहाँ हम इस शब्द को लेकर विवाद में नहीं पड़ना चाहते। इस सम्बन्ध में श्री निहालचन्द जी ने अपनी पुस्तक ‘वैश्य-अग्रवाल राजवंश समाज का इतिहास’ में पृष्ठ 40 पर जो लिखा है वह हम स्वीकार करते हैं। उनके शब्द हैं, ‘उपरोक्त समस्त उल्लेखों और तथ्यों का गहराई से अध्ययन करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि राजवंश अग्रवाल समाज उसी परम्परा से जुड़ा है, जिसमें कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन ने राजकन्याओं और नागकन्याओं की सन्तानों को उनकी
अलग-अलग पहचान के लिए राजवंशी और नागवंशी संस्तरणों में रखा था। तब से यह लोग इन्हीं नामों से अंकित होते आए हैं। अठारहवीं शताब्दी में राजवंशियों में एक प्रतापी वीर पुरुष राजा रतनचंद के नाम से हुए जिन्होंने मुगल दरबार में उच्च पद प्राप्त किया और उस काल में अत्यन्त प्रभावशाली एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कट्टरपंथी एवं रुढ़िवादी लोगों के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके साथ परिवारों और व्यक्तियों के समूह जुड़ते चले गए और इस प्रकार
-----------------------------------
1. डॉ. स्वराज्य मणिअग्रवाल-‘अग्रसेन, अग्रवाल, अग्राहा’, पृष्ठ 180
2. ‘वैश्य-अग्रवाल राजवंश समाज का इतिहास’ पृष्ठ-38
जिन लोगों ने उनका साथ दिया वे ‘राजा की बिरादरी’ और ‘राजाशाही’ के नाम से अंकित हुए और आगे चल कर उन्होंने अपना पुराना नाम ‘राजवंशी’ ही धारण कर लिया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि राजा रतनचंद्र एक ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, जिन्होंने राजवंश अग्रवाल समाज को गौरवान्वित किया, किन्तु जो समाज उनसे पहले से ही चला आ रहा था, उसका उन्हें प्रवर्तक बताना तो अतिशयोक्ति ही होगी क्योंकि राजवंशी अग्रवाल के आदि पुरुष या प्रवर्तक तो राजा अग्रसेन ही हैं।
अन्तिम मुगलों के इतिहास मुगलों के इतिहास में सैयद बंधुओं और राजा रतनचंद का क्या रोल रहा है और कितना प्रभाव था उनका, इसको लेकर हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेन्द्र वर्मा ने एक बहुत सुन्दर नाटक लिखा है, ‘छोटे सैयद बड़े सैयद।’ इस नाटक को पढ़ते हुए और देखते हुए हम सही रूप में राजा रतनचंद की योग्यता और शक्ति से परिचित हो सकते हैं। सैयद बंधुओं की सफलता के पीछे राजा रतनचंद का ही मस्तिष्क था। वह न होते तो सैयद बंधु आपस में लड़कर मर जाते। समय-समय पर उन्होंने कैसे दोनों भाइयों के बिगड़ते सम्बन्धों को सुधारा और राजनीति की कैसी-कैसी
विलक्षण चालें चलीं, यह सब नाटक को पढ़कर ही जाना जा सकता है। वे शासन प्रणाली में भी बहुत कुशल थे लेकिन सैयद बंधुओं का जो स्वप्न था वह पूरा नहीं हुआ और षड्यंत्र करने वाले खुद ही राजदरबार के षड्यन्त्रों में उलझ गए। अन्त में मोहम्मद शाह ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। छोटे सैयद की पहले ही हत्या हो चुकी थी। अन्तिम युद्ध में अब्दुल्ला और रतनचंद की फौजें भी हार गईं और उनके साथी सब गिरफ्तार कर लिए गए। उन सब बंदियों को सज़ा देते हुए मोहम्मद शाह की दृष्टि सबसे पहले राजा रतनचंद पर पड़ती है। वह पूछते हैं, ‘राजा रतनचंद, आपको अपने बारे में कुछ कहना है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book