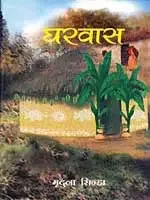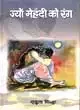|
सामाजिक >> घरवास घरवासमृदुला सिन्हा
|
220 पाठक हैं |
||||||
निरंतर परिवर्तित होते ग्रामीण गृहस्थ जीवन में कृषकों मजदूरों और स्त्रियों की संघर्षमय जीवटता की अद्भुत गाथा...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
घरवास निरंतर परिवर्तित होते ग्रामीण गृहस्थ जीवन में कृषकों मजदूरों और
स्त्रियों की संघर्षमय जीवटता की अद्भुत गाथा है, जिसमें रामपुरा गाँव को
केंद्र में रखकर पूरे उत्तर बिहार की आंचलिक विशिष्टताओं की झाँकी
प्रस्तुत हुई है तो दूसरी ओर वही से पंजाब प्रांत के नैसर्गिक सौंदर्य पर
आतंकवादी गतिविधियों की पड़ी कलुषित छाया के दर्द और दंश को रेखांकित कर
भारतीय प्रांतों की परस्पर निर्भरता को दरशाया गया है।
लेखनी क्या-क्या कहे....
मात्र समाचार पढ़ और सुनकर नहीं, अँखियन देखा है तब के पंजाब में डरी,
सहमी, काँपती-थर्राती और सिसकती सतलज एवं व्यास को; तथा बिहार
में विचलित सी कभी बड़बड़ाती, कभी बिलखती और कभी विवश बागमती। तभी तो
वेगवती बागमती के कगार बंधनहीन हैं। मजबूर है बागमती। स्नेहवश इतना उमड़ती
रही है कि उसके स्नेहभाजक बिहार के मजदूर और छोटे किसानों को दर-ब-दर होना
पड़ा है। पापी पेट की खातिर अपने ‘देस से बाहर अपने लोगों का
बिछोह मन में छुपाए वे जहाँ गए, उसी को अपनत्व से सजाने-सँवारने में जुट
गए—कभी सागर का मॉरीशस, गायना, फिजी तो कभी अपने ही
‘देस’ में परदेसिया बनकर असम, बंगाल के चाय बागान,
भीड़ भरी कलकत्ता नगरी और अब ‘पुरबिया’ और
भय्यन’ बनकर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में।
पंजाब की पीली सरसों और गेहूँ-धान की सुनहरी फसलें इन्हें सम्मोहित करती हैं। सम्मोहित है पंजाब भी इनकी मेहनत, ईमानदारी और भोलेपन पर। पसीने से तर-बतर ये आटा गूँध ही रहे होते थे कि इनका खून बहा दिया जाता था। जो यहाँ किसी तरह बच जाते थे वे वापस गाँव पहुँचते-पहुँचते परंपरागत सामंती सोच में पले-पुसे नवधनिकों के मोह कुचक्र से कट-छँटकर आधे-पौने रह जाते हैं।
व्यास और बागमती के जल से सिंचित भारत माँ के दो हिस्सों के मध्य सेतुस्वरूप इन अँखफोड़ हुए मजदूरों को अब अस्मिता और सम्मान के साथ जीवन की तलाश है। अपना घर, अपनी छत; जिसके नीचे श्रम से चूर शरीर का अपना मन हो। परंतु कहाँ नसीब होता है सबको अपना घर ! अपने नसीब को बदलने, रोटी-कपड़ा के उपरांत अपना घर बनाने में क्या-क्या नहीं झेलना पड़ता है इन मजदूरों को।
सरकारी अनुकंपा से बने एक कमरे के घर को दिखाती कलिया की आँखों में सबकुछ उतर आता है—उल्लास, उमंग के साथ-साथ नींव से लेकर कँगूरे के निर्माण तक के संघर्ष की गाथा। राजनीतिक लाभ के अघाए भुक्खड़ों द्वारा फेंके जाल में फँसते जाने की मजबूरी। और उस अथाह मन में डुबकी लगाने पर हाथ लगा एक तिनका—उनके नवजात आत्मविश्वास का।
यह दुर्बल लेखनी क्या-क्या बखाने-विलोचना की विलक्षण शक्ति को या उस पर हो रहे दोतरफा अत्याचारों को ? डाक बाबू की डाकेजनी या अँधेरे परिवेश में जुगनुओं की मानिंद रामजीवन सिंह और नरेंद्र को ? या कि ‘सफेद गिद्धों’ के जाल में फँसे आत्मघात के लिए विवश विजय को ? या उस गाँव में गाँधीवाद की अंतिम कड़ी, धू-धू कर जले बिलट माझी को ? गिरी-पड़ी-जली मड़ैयों को या ऊँची चौखटों में घुलते नींववाले मकानों को ? छतविहीन घरों को या चौंक-चौंककर खुलती नींदों को ? हवा में तैरते भय को या गलियों में रेंगते सन्नाटे को ? सरकारी विकास परियोजनाओं के थमे गँदले जल में पैदा हुए नवधनिक ठेकेदार राघव मिश्र को या व्यास का जल बागमती में मिलाने को उद्यत विलोचना के जलाए गए घर की मातमपुरसी करने आए सरदार करतारसिंह को ? गाँव में नित उठे फसादौं को चौके-चूल्हे पर पका-पकाकर स्वादिष्ट बनाती रामलखी और और दुलरिया को या पोथी-पतरा से पेट थामे, नव परिवर्तन का पाठ पढ़ते पंडितजी को ? इन सारी विसंगतियों में जनमी कलिया की निर्भीकता और विद्रोह को, जो पंडित और पोथी के बगैर भी घरवास की रस्म पूरी करती है ?
कहानी सुनाने की कोई चाहत नहीं थी। सिर्फ उनकी सुनी थी। तथ्य इकट्ठे किए थे। उनके अंतर्मन के भावों को भाषा देते ही सबकुछ कथानक में बदल रहा है...
पंजाब की पीली सरसों और गेहूँ-धान की सुनहरी फसलें इन्हें सम्मोहित करती हैं। सम्मोहित है पंजाब भी इनकी मेहनत, ईमानदारी और भोलेपन पर। पसीने से तर-बतर ये आटा गूँध ही रहे होते थे कि इनका खून बहा दिया जाता था। जो यहाँ किसी तरह बच जाते थे वे वापस गाँव पहुँचते-पहुँचते परंपरागत सामंती सोच में पले-पुसे नवधनिकों के मोह कुचक्र से कट-छँटकर आधे-पौने रह जाते हैं।
व्यास और बागमती के जल से सिंचित भारत माँ के दो हिस्सों के मध्य सेतुस्वरूप इन अँखफोड़ हुए मजदूरों को अब अस्मिता और सम्मान के साथ जीवन की तलाश है। अपना घर, अपनी छत; जिसके नीचे श्रम से चूर शरीर का अपना मन हो। परंतु कहाँ नसीब होता है सबको अपना घर ! अपने नसीब को बदलने, रोटी-कपड़ा के उपरांत अपना घर बनाने में क्या-क्या नहीं झेलना पड़ता है इन मजदूरों को।
सरकारी अनुकंपा से बने एक कमरे के घर को दिखाती कलिया की आँखों में सबकुछ उतर आता है—उल्लास, उमंग के साथ-साथ नींव से लेकर कँगूरे के निर्माण तक के संघर्ष की गाथा। राजनीतिक लाभ के अघाए भुक्खड़ों द्वारा फेंके जाल में फँसते जाने की मजबूरी। और उस अथाह मन में डुबकी लगाने पर हाथ लगा एक तिनका—उनके नवजात आत्मविश्वास का।
यह दुर्बल लेखनी क्या-क्या बखाने-विलोचना की विलक्षण शक्ति को या उस पर हो रहे दोतरफा अत्याचारों को ? डाक बाबू की डाकेजनी या अँधेरे परिवेश में जुगनुओं की मानिंद रामजीवन सिंह और नरेंद्र को ? या कि ‘सफेद गिद्धों’ के जाल में फँसे आत्मघात के लिए विवश विजय को ? या उस गाँव में गाँधीवाद की अंतिम कड़ी, धू-धू कर जले बिलट माझी को ? गिरी-पड़ी-जली मड़ैयों को या ऊँची चौखटों में घुलते नींववाले मकानों को ? छतविहीन घरों को या चौंक-चौंककर खुलती नींदों को ? हवा में तैरते भय को या गलियों में रेंगते सन्नाटे को ? सरकारी विकास परियोजनाओं के थमे गँदले जल में पैदा हुए नवधनिक ठेकेदार राघव मिश्र को या व्यास का जल बागमती में मिलाने को उद्यत विलोचना के जलाए गए घर की मातमपुरसी करने आए सरदार करतारसिंह को ? गाँव में नित उठे फसादौं को चौके-चूल्हे पर पका-पकाकर स्वादिष्ट बनाती रामलखी और और दुलरिया को या पोथी-पतरा से पेट थामे, नव परिवर्तन का पाठ पढ़ते पंडितजी को ? इन सारी विसंगतियों में जनमी कलिया की निर्भीकता और विद्रोह को, जो पंडित और पोथी के बगैर भी घरवास की रस्म पूरी करती है ?
कहानी सुनाने की कोई चाहत नहीं थी। सिर्फ उनकी सुनी थी। तथ्य इकट्ठे किए थे। उनके अंतर्मन के भावों को भाषा देते ही सबकुछ कथानक में बदल रहा है...
घरवास
* एक *
...रामजीवन सिंह का दरवाजा। एक हजार की आबादीवाले उस छोटे से गाँव के
बीचोबीच स्थित चार कमरों के घर का दरवाजा—जमीन से चार फिट ऊँचा।
और उस ऊँचाई पर खाट में धँसी बैठी रामजीवन सिंह की माँ चरवाहे को ऊँची
आवाज में आज्ञा दे रही थीं, ‘‘जल्दी कर, बैल को घर
में बाँध। बालटी ले आ। गाय दुहनेवाला आता ही होगा।’’
उनकी यही संध्यचर्या है। चरवाहे से काम लेने की जल्दबाजी के पीछे मात्र साँझ का पीछा करते आ रहे अँधियारों का डर नहीं होता। उन्हें तो ऊब होती है दरवाजे की शोभा बढ़ाती शाम की बैठकी से। दिन छुपते ही गाँव के चारों कोनों से लोग उनके दरवाजे की ओर सरकने लगते हैं। उनके सुपुत्र रामजीवन सिंह उर्फ मास्टर साहब शहर से लौटते वक्त समाचार पत्र ले आते हैं। मास्टर साहब को भी समाचार पत्रों में छपी खबरों को अपने ग्रामीण-बंधु-बांधवों में बाँटने में रस आता है। वैसे काफी मँहगा शौक है यह। घर में उनकी बूढ़ी माँ, पत्नी, पन्द्रह वर्षीया एक बेटी सुषमा है। इन दिनों तो बेटा भी दिल्ली से आया हुआ है। दरवाजे पर बैठे-बैठे देश-दुनिया की चर्चा करना और चाय के लिए बार-बार अंदर खबर भिजवाना उनका नियम बन गया है। उस दरवाजे पर प्रति शाम बैठती सभा के कुछ लोग तो स्थायी सदस्य हैं, जिन्हें चाय की चुस्की के साथ समाचार पत्र चबाने का चस्का लग गया है।
‘‘रे छोरा ! क्या खेल करने लगा ? आज ठहर। मालिक आते ही होंगे। तेरी मरम्मत करवाती हूँ।’’ माताजी ने फिर चरवाहे को डाँट लगाई।
देवता सिंह के आने का समय हो चुका था, इसलिए आ ही गए। बोले, ‘‘भौजी, आज किसकी मरम्मत हो रही है ?’’
देवता सिंह बैठकी के स्थायी सदस्य हैं। उनकी आवाज सुनकर माताजी को संध्या गहराने का आभास हुआ। झल्लाकर बोलीं, ‘‘अभी तो बबुआ आया नहीं।’’
एक तो बेटे को लौटने में विलंब होने से उत्पन्न दुःशंका, दूसरे इन समाचार-प्रेमियों की बैठकों से चिढ़ में डूबती-उतराती माताजी को देवता सिंह का आगमन सुहाया नहीं था। उन्होंने अपनी बेरुखी से उन्हें टालना चाहा। पर देवता सिंह टलें तो जाएं कहाँ ? वे तो अपने दरवाजे का काम निबटाकर आए थे।
‘‘आते ही होंगे। शहर में कोई विशेष घटना घट गई होगी। पूरी छानबीन करके आएँगे न। कॉलेजिया छोकरों की तरह हवा में उड़ती खबर तो वे कभी लाते नहीं।’’ देवता सिंह दरवाजे पर रखी चौकी के अपने निश्चित स्थान पर दोनों पाँव ऊपर कर निश्चिंतता से बैठते हुए बोले।
माताजी क्या करतीं ? एक बार पुनः चरवाहे को दी गई आज्ञा दुहराकर अपने देवरजी के पास बैठ गईं। बोलीं, ‘‘बबुआजी ! आपको तो याद होगा, आपके भाई साहब कहा करते थे कि अखबार में ज्यादा झूठ-फूस बातें छपती हैं। मुझे तो लगता है कि कुछ तो झूठी खबरें होती हैं और कुछ खबरों को बढ़ा-चढ़ाकर छापा जाता है। अखबार रोज चार पन्ने का ही छपता है। क्या दुनिया भर में सब दिन उतनी ही घटना-दुर्घटनाएँ होती हैं ? किसी दिन कम या किसी दिन ज्यादा भी तो हो सकती हैं न !’’
अपने भाई के जमाने से ही भाभी की हाँ में हाँ मिलाने की देवता सिंह की लत अब उनकी उम्र के साथ बूढी हो चली है। उनकी समर्थन भरी मुसकान ने उनकी भाभी को आगे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, ‘‘बबुआ, एक बात पर विचार कीजिए। जब से पढ़ाई-लिखाई का चलन हुआ है तब से समाज में झूठ-प्रपंच भी बढ़ने लगा। कागज सस्ता हो गया। किताब-कॉपी छपने लगी। अब तो सब जात के लोग अपने लड़िकन को पढ़ाने लगे। पढ़ल-लिखल लोग खेतीबाड़ी भी करना नहीं चाहते। सबको नौकरी तो मिलती नहीं। ‘बैठल बनियाँ क्या करे, इस कोठी का धान-चावल उस कोठी करे।’ तभी तो रोज दिन बहुबात उठती है।’’
देवता सिंह ठहाका लगाकर हँस पड़े। माताजी की बातों में गाँव के नौजवानों को भी रस आता है। वे अपनी बूढ़ी दादी को छेड़ छेड़कर उनकी दलीलें सुना करते हैं। माताजी को नए जमाने के नए रस्म-रिवाजों और जबरदस्ती अख्तियार किए गए व्यसनों से चिढ़ है। समाचारपत्र पढ़ने, नौकरी करने, परदेस जाने, लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई के विरोध में उनके अपने ठोस विचार हैं।
विजय आ गया था। देवता सिंह की हँसी में सहयोग देकर बोला, ‘‘आपका बेटा और पोता भी तो पढ़े-लिखे हैं। क्या वे दोनों भी...’’
‘‘वही दोनों कौन सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं ! पढ़ेगा-लिखेगा तो झूठ-फरेब करना ही पड़ेगा।’’ माताजी ने अपनी पकी-पकाई दलील रखी। परंतु अँधेरा घिर आने के आभास के साथ उनकी चिंता जीवित हो उठी। बोलीं, ‘‘देखो ! अब तक दोनों नहीं आए। जमाना खराब हो गया। रात-बिरात चलने लायक राह रहा नहीं। साँझ होते ही मुझे चिंता होने लगती है। लोग दिन-दहाड़े आदमी को बकरी-मुरगी की तरह काटने लगे हैं।’’
चिंतित भाभी की चिंता करते हुए देवतासिंह ने कहा, ‘‘नाहक परेशान हैं आप ! आज भी तो व्यक्ति दूसरे का बिगाड़ न करे तो उसका बाल भी बाँका नहीं होता। भगवान् पर विश्वास रखिए।’’
विजय ने तो आज अपनी दादी के विचार की उलटी धारा में डुबकी भी नहीं लगाई थी। उसने दादी को छेड़ा, ‘‘दादी, आज तो लड़कियाँ भी पड़ने लगीं। अपने ही गाँव में देखिए न ! अपनी जाति का कोई घर है, जिसकी कोई-न-कोई बहू या बेटी मास्टरनी या दूसरी नौकरी में नहीं है ?’’
‘‘हाँ, बेटा, किसी-किसी घर में तो तीन-चार मास्टरनियाँ हैं। केवल मर्द लोग पढ़ें तो एक बात भी है। लड़कियों को पढ़ाओ और उन्हें भी नौकरी दिलाओ। मुझे लगता है कि औरतें नौकरी नहीं करतीं तो पढ़-लिखकर तुम्हारी तरह कोई मर्द भी बेकार नहीं रहता। मर्दों के बराबर तो औरतें नौकरी लेने लगी हैं। तुम लोग बेकार बैठोगे ही।’’
विजय को अपनी दादी के विचार सुनकर अचंभा हुआ। लेकिन दादी को छेड़ने के लिए ही वह बोला, ‘‘दादी, आप भी तो औरत हैं। औरत के खिलाफ कैसे बोलती हैं ?’’
‘‘अरे बचवा ! हम किसी के खिलाफ नहीं। हम तो घर-घर की खैरियत की बात सोचते हैं। अब देखो न, इसी गाँव की क्या हालत है ! जरा सोचो। बोलिए न बबुआजी ! आज मुंह में दही जमाकर क्यों बैठे हैं ?’’
विजय ठहाका लगाकर हँस पड़ा, ‘‘दही नहीं, दादी, खैनी (सुरती) होगी।’’ देवतासिंह दरवाजे के किनारे जाकर थूक फेंक आए और बोले, ‘‘नहीं, मैं तो भौजी के विचार सुन रहा था। कहीं विरोध हो तो बोलूँ। ठीक ही कह रही थीं भौजी। इस इलाके में भी अपना गाँव शिवजी के त्रिशूल पर बसा है। दोपहर में गाँव को एक छोर से दूसरे छोर तक घूम आओ तो मुरदों का गाँव लगता है। अपना काम-धन्धा निपटाकर मर्द लोग तो नौकरी पर चले जाते हैं। दूरा—दरवाजा सूना तो होगा ही। मेरी तरह निठल्ले लोग गाँव-भर में दस-पाँच ही तो बचे।’’
देवता सिंह की बात को ही विस्तार दिया माताजी ने, ‘‘आप तो दूरा-दरवाजा की बात करते हैं, घर की औरतें भी तो चली जाती हैं। अपने गाँव के चारों स्कूलों में कितनी देवीजी हैं ?’’
‘‘मैंने गिनती कर रखी है, दादी। प्राइमरी स्कूल में चार, मिडिल स्कूल में पाँच और कन्यापाठ शाला में तो सात-की-सात देवियाँ हैं ही। हाई-स्कूल में भी अब चार हो गईं। और इसके अलावा अपने गाँव की चारों सीमाओं पर बसे गाँवों में भी तो अपने गाँव की औरतें मास्टरनी हैं। कुल मिलाकर पचास मास्टरनी हैं अपने गाँव की।’’
‘‘दुर ! तू भी झूठ ही बोलने लगा। पढ़ा-लिखा है न।’’ दादी ने प्यार भरी झिड़की दी विजय को।
‘‘नहीं, भौजी ! आप समझी नहीं। अपने गाँव की बेटियाँ जो दूसरे गाँवों में ब्याही हैं, और वहाँ जाकर मास्टरनी बनीं, उनके् नाम भी जोड़ लिये विजय ने। देवता सिंह से अपने अनुसार गिनती कर ली।
‘‘तब तो और भी झूठ है। बाप रे ! बीस-पच्चीस बरस में तो न जाने कितनी लड़कियाँ ट्रेनिंग करके ससुराल गईं। लेकिन एक बात है। ट्रेनिंग की हुई लड़की की शादी का झमेला नहीं होता। दूसरे गाँव के लोग भी तो मास्टरनी बहू चाहते हैं। तिलक-दहेज ज्यादा नहीं मिला तो भी क्या, मास्टरनी तो मिलती है।’’
भाभी का समर्थन किया देवता सिंह ने, ‘‘क्यों नहीं ! बुढ़ापे तक अपने खूँटे से कामधेनु गाय बांधे रखते हैं।’’
माताजी देवता सिंह की उपमा की तह तक न जाकर बोल पड़ीं, ‘‘कुछ भी कहिए, मुझे औरतों का गाँव-घर से पैर बाहर निकालना अच्छा नहीं लगता। मास्टरनी अब तो ससुर–भैंसुर के आगे पैर निकालकर चलती ही थीं, अब तो अस्पताल में भी जाकर पता नहीं क्या काम करने लगी हैं औरतें !’’
‘‘मिडवाइफ और नर्स हो रही हैं, दादी। बच्चा पैदा करवाती हैं और रोगी की सेवा-शुश्रूषा करती हैं। अच्छी तनख्वाह मिलती है और ऊपर से इनाम, बख्शीश भी।’’
‘‘मारो झाड़ू से। ये सब काम कहीं भले घर की बहू-बेटियों का है ! छिह ! छिह !! पैसा की खातिर मर्द लोग क्या-क्या करवाने लगे अपनी औरतों से; मुझे अच्छा नहीं लगता। मर्द ही नाच नचाते हैं।’’
थोड़ी देर चुप्पी बनी रही। माताजी ने फिर कहा, ‘‘बबुआ नहीं आए ! बड़ी देर हो गई !’’
‘‘दादी, आप अच्छा-खासा भाषण दे लेती हैं। अगली बार चुनाव में आपको विरोधी दल का उम्मीदवार बनाया जा सकता है।’’ विजय ने हँसते हुए कहा।
पर जब तक माताजी विजय की बात समझतीं और चुनाव पर अपना मत व्यक्त करतीं, उनके पुत्र रामजीवन सिंह आ गए। माताजी ने राहत की साँस ली।
रामजीवन सिंह ने विजय की आधी बात सुन ली थी। पूछा, ‘‘किसे उम्मीदवार बना रहे हो ?’’
‘‘भौजी को ! देवता सिंह ने कहा।
दरवाजे पर बैठे सब लोगों की मिली-जुली हँसी गूँज उठी है।
विजय हँसते हुए बोला, ‘‘चाचा, दादी विरोधी दल के नेता के नाते अच्छा भाषण दे सकती हैं। अभी एक घंटा से समाचार पत्र, पढ़ाई लिखाई, नौकरी-चाकरी के विरोध में बोल रही थीं।’’
पुनः हँसी की फुहार बरसने के पहले ही रामजीवन सिंह की मुद्रा देख थम गई।
देवता सिंह ने पूछा, ‘‘क्या समाचार है बबुआ ?’’
‘‘बहुत खराब !’’ रामजीवन सिंह के दो शब्द उसके मन की गहन चिंता से सराबोर थे।
‘‘क्या हुआ ?’’ माताजी ने उत्कंठा जताई, ‘‘अखबार पढ़कर सुना तो ! देश-दुनिया में सब ठीक है न ?’’
समाचार सुनने की उनकी उत्सुकता ने सबको विस्मित कर दिया।
‘‘नहीं, माँ ! ठीक-ठाक कैसे होगा ! पंजाब की समस्या गहराती जा रही है। कल आतंकवादियों ने एक बस से दस लोगों को खींचकर मारा है। उनमें आठ तो बिहारी मजदूर थे।’’
खबर सुनते-सुनाते रामजीवन सिंह का स्वर भारी हो उठा। स्थिति की गंभीरता ने सबको अपने में लपेट लिया।
चुप्पी भंग की विजय ने, ‘‘चाचा, मरनेवालों के नाम भी लिखे हैं ?’’
जवाब में रामजीवन सिंह ने विजय की ओर अखबार बढ़ा दिया।
समाचारपत्र पढ़ने की बात आई तब सबके सब लालटेन की खोज करने लगे। रामजीवन सिंह झल्लाए, ‘‘अब तक लालटेन भी नहीं जलाई ?’’
‘‘अरी सुष्मी ! जरा लालटेन जला के लाना।’’ दादी ने पोती को आज्ञा देकर कहा, ‘‘अरे बेटा ! ऐसी टहटही इँजोरिया (साफ चाँदनी) में साँझे से क्या लालटेन जलाएँ। किरासन तेल भी तो नहीं मिलता। किना महँगा है ! कु्आँ-पोखर से तो नहीं खिंचता है न तेल। मोल लेना पड़ता है। बज्र पड़े बिजली की लाइन में ! नाम के लिए है। कभी-कभी भुक-भुक कर जाती है।’’
सब जानते हैं कि माँ के आगे रामजीवन की एक नहीं चलती। उनकी खेती-बाड़ी, माल-मवेशी और घर-द्वार—सबकुछ तो माँ ही सँभालती हैं। घर की मालिक और मालकिन वही आई हैं रामजीवन सिंह को अपनी मास्टरी और सामाजिक कार्यों से फुरसत ही कहाँ मिलती है ! उनकी पत्नी को इस घर में बहू बनकर आए तीस बरस बीत गए। अब अपनी भी बहू आनेवाली है; पर अब तक सास का हुक्म बजाती आई है, मालकिन नहीं बन पाई।
विजय अन्दर गया और लालटेन ले आया। समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ पर ही लिखा समाचार सुन श्रोताओं के दिल दहल गए। सबके सब चुप।
‘‘और जाएँ पंजाब। काटें गेहूँ। खाएँ मालपुआ। समझा-बुझा के कहे—रे, पंजाब न जा। अपने गाँव की धरती को जोतो, कोड़ों; जो रूखा-सूखा मिले, खा—पीकर गुजर करो। बाल-बच्चे के साथ रहोगे। कौन माने मेरी बात !’’ रामजीवन सिंह की माँ अपने गाँव के तमाम मुसहर, धोबी, चमार—जो पिछले कई वर्षों से पंजाब जाते रहे हैं, उनपर झुँझला उठीं। उनकी झल्लाहट में अपने ग्रामीण मजदूरों के लिए अपनेपन में सना क्रोध था, मरनेवालों के प्रति वेदना थी।
‘‘भौजी, पंजाब न जाते तो रेडियो कैसे बजाते ? मुसहरनी सब छींट की साड़ी कैसे पहनतीं ? अरे, बाप रे ! कैसी-कैसी लहकदार साड़ियाँ पहनकर गाँव भर में घूमती हैं ! अब तो हम लोगों से भी कोई लाज, न शरम।’’ देवता सिंह ने मुसहरनियों के प्रति अपने मन का गुबार निकाला।
अगर रामजीवन सिंह पंजाब की स्थिति की गंभीरता की ओर ध्यान नहीं खींचते तो सबके सब अपने गाँव के मजदूरों के ऊपर ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रह जाते और उनकी माताजी की सभाध्यक्षता बनी रहती।
‘‘भई, गाँव में काम नहीं मिलता तो पंजाब, असम या कलकत्ता क्यों नहीं जाएँ ? आखिर पेट तो पालना ही है। गाँव में भूखों मरने से अच्छा है, कहीं जाकर रोटी कमाना। कुछ ही वर्षों से तो पंजाब जाने लगे हैं। बिहार के मजदूर तो पहले असम, कलकत्ता जाते रहे। असमियों ने हो-हल्ला मचाया तो अब उन्होंने अपने पैरों की दिशा पूरब से उत्तर-पश्चिम कर ली। अब पंजाबवालों ने मारना शुरू किया है—
आगे-आगे देखो, होता है क्या ?’’ रामजीवन सिंह के पीड़त मन के बोल थे।
उनकी यही संध्यचर्या है। चरवाहे से काम लेने की जल्दबाजी के पीछे मात्र साँझ का पीछा करते आ रहे अँधियारों का डर नहीं होता। उन्हें तो ऊब होती है दरवाजे की शोभा बढ़ाती शाम की बैठकी से। दिन छुपते ही गाँव के चारों कोनों से लोग उनके दरवाजे की ओर सरकने लगते हैं। उनके सुपुत्र रामजीवन सिंह उर्फ मास्टर साहब शहर से लौटते वक्त समाचार पत्र ले आते हैं। मास्टर साहब को भी समाचार पत्रों में छपी खबरों को अपने ग्रामीण-बंधु-बांधवों में बाँटने में रस आता है। वैसे काफी मँहगा शौक है यह। घर में उनकी बूढ़ी माँ, पत्नी, पन्द्रह वर्षीया एक बेटी सुषमा है। इन दिनों तो बेटा भी दिल्ली से आया हुआ है। दरवाजे पर बैठे-बैठे देश-दुनिया की चर्चा करना और चाय के लिए बार-बार अंदर खबर भिजवाना उनका नियम बन गया है। उस दरवाजे पर प्रति शाम बैठती सभा के कुछ लोग तो स्थायी सदस्य हैं, जिन्हें चाय की चुस्की के साथ समाचार पत्र चबाने का चस्का लग गया है।
‘‘रे छोरा ! क्या खेल करने लगा ? आज ठहर। मालिक आते ही होंगे। तेरी मरम्मत करवाती हूँ।’’ माताजी ने फिर चरवाहे को डाँट लगाई।
देवता सिंह के आने का समय हो चुका था, इसलिए आ ही गए। बोले, ‘‘भौजी, आज किसकी मरम्मत हो रही है ?’’
देवता सिंह बैठकी के स्थायी सदस्य हैं। उनकी आवाज सुनकर माताजी को संध्या गहराने का आभास हुआ। झल्लाकर बोलीं, ‘‘अभी तो बबुआ आया नहीं।’’
एक तो बेटे को लौटने में विलंब होने से उत्पन्न दुःशंका, दूसरे इन समाचार-प्रेमियों की बैठकों से चिढ़ में डूबती-उतराती माताजी को देवता सिंह का आगमन सुहाया नहीं था। उन्होंने अपनी बेरुखी से उन्हें टालना चाहा। पर देवता सिंह टलें तो जाएं कहाँ ? वे तो अपने दरवाजे का काम निबटाकर आए थे।
‘‘आते ही होंगे। शहर में कोई विशेष घटना घट गई होगी। पूरी छानबीन करके आएँगे न। कॉलेजिया छोकरों की तरह हवा में उड़ती खबर तो वे कभी लाते नहीं।’’ देवता सिंह दरवाजे पर रखी चौकी के अपने निश्चित स्थान पर दोनों पाँव ऊपर कर निश्चिंतता से बैठते हुए बोले।
माताजी क्या करतीं ? एक बार पुनः चरवाहे को दी गई आज्ञा दुहराकर अपने देवरजी के पास बैठ गईं। बोलीं, ‘‘बबुआजी ! आपको तो याद होगा, आपके भाई साहब कहा करते थे कि अखबार में ज्यादा झूठ-फूस बातें छपती हैं। मुझे तो लगता है कि कुछ तो झूठी खबरें होती हैं और कुछ खबरों को बढ़ा-चढ़ाकर छापा जाता है। अखबार रोज चार पन्ने का ही छपता है। क्या दुनिया भर में सब दिन उतनी ही घटना-दुर्घटनाएँ होती हैं ? किसी दिन कम या किसी दिन ज्यादा भी तो हो सकती हैं न !’’
अपने भाई के जमाने से ही भाभी की हाँ में हाँ मिलाने की देवता सिंह की लत अब उनकी उम्र के साथ बूढी हो चली है। उनकी समर्थन भरी मुसकान ने उनकी भाभी को आगे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, ‘‘बबुआ, एक बात पर विचार कीजिए। जब से पढ़ाई-लिखाई का चलन हुआ है तब से समाज में झूठ-प्रपंच भी बढ़ने लगा। कागज सस्ता हो गया। किताब-कॉपी छपने लगी। अब तो सब जात के लोग अपने लड़िकन को पढ़ाने लगे। पढ़ल-लिखल लोग खेतीबाड़ी भी करना नहीं चाहते। सबको नौकरी तो मिलती नहीं। ‘बैठल बनियाँ क्या करे, इस कोठी का धान-चावल उस कोठी करे।’ तभी तो रोज दिन बहुबात उठती है।’’
देवता सिंह ठहाका लगाकर हँस पड़े। माताजी की बातों में गाँव के नौजवानों को भी रस आता है। वे अपनी बूढ़ी दादी को छेड़ छेड़कर उनकी दलीलें सुना करते हैं। माताजी को नए जमाने के नए रस्म-रिवाजों और जबरदस्ती अख्तियार किए गए व्यसनों से चिढ़ है। समाचारपत्र पढ़ने, नौकरी करने, परदेस जाने, लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई के विरोध में उनके अपने ठोस विचार हैं।
विजय आ गया था। देवता सिंह की हँसी में सहयोग देकर बोला, ‘‘आपका बेटा और पोता भी तो पढ़े-लिखे हैं। क्या वे दोनों भी...’’
‘‘वही दोनों कौन सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं ! पढ़ेगा-लिखेगा तो झूठ-फरेब करना ही पड़ेगा।’’ माताजी ने अपनी पकी-पकाई दलील रखी। परंतु अँधेरा घिर आने के आभास के साथ उनकी चिंता जीवित हो उठी। बोलीं, ‘‘देखो ! अब तक दोनों नहीं आए। जमाना खराब हो गया। रात-बिरात चलने लायक राह रहा नहीं। साँझ होते ही मुझे चिंता होने लगती है। लोग दिन-दहाड़े आदमी को बकरी-मुरगी की तरह काटने लगे हैं।’’
चिंतित भाभी की चिंता करते हुए देवतासिंह ने कहा, ‘‘नाहक परेशान हैं आप ! आज भी तो व्यक्ति दूसरे का बिगाड़ न करे तो उसका बाल भी बाँका नहीं होता। भगवान् पर विश्वास रखिए।’’
विजय ने तो आज अपनी दादी के विचार की उलटी धारा में डुबकी भी नहीं लगाई थी। उसने दादी को छेड़ा, ‘‘दादी, आज तो लड़कियाँ भी पड़ने लगीं। अपने ही गाँव में देखिए न ! अपनी जाति का कोई घर है, जिसकी कोई-न-कोई बहू या बेटी मास्टरनी या दूसरी नौकरी में नहीं है ?’’
‘‘हाँ, बेटा, किसी-किसी घर में तो तीन-चार मास्टरनियाँ हैं। केवल मर्द लोग पढ़ें तो एक बात भी है। लड़कियों को पढ़ाओ और उन्हें भी नौकरी दिलाओ। मुझे लगता है कि औरतें नौकरी नहीं करतीं तो पढ़-लिखकर तुम्हारी तरह कोई मर्द भी बेकार नहीं रहता। मर्दों के बराबर तो औरतें नौकरी लेने लगी हैं। तुम लोग बेकार बैठोगे ही।’’
विजय को अपनी दादी के विचार सुनकर अचंभा हुआ। लेकिन दादी को छेड़ने के लिए ही वह बोला, ‘‘दादी, आप भी तो औरत हैं। औरत के खिलाफ कैसे बोलती हैं ?’’
‘‘अरे बचवा ! हम किसी के खिलाफ नहीं। हम तो घर-घर की खैरियत की बात सोचते हैं। अब देखो न, इसी गाँव की क्या हालत है ! जरा सोचो। बोलिए न बबुआजी ! आज मुंह में दही जमाकर क्यों बैठे हैं ?’’
विजय ठहाका लगाकर हँस पड़ा, ‘‘दही नहीं, दादी, खैनी (सुरती) होगी।’’ देवतासिंह दरवाजे के किनारे जाकर थूक फेंक आए और बोले, ‘‘नहीं, मैं तो भौजी के विचार सुन रहा था। कहीं विरोध हो तो बोलूँ। ठीक ही कह रही थीं भौजी। इस इलाके में भी अपना गाँव शिवजी के त्रिशूल पर बसा है। दोपहर में गाँव को एक छोर से दूसरे छोर तक घूम आओ तो मुरदों का गाँव लगता है। अपना काम-धन्धा निपटाकर मर्द लोग तो नौकरी पर चले जाते हैं। दूरा—दरवाजा सूना तो होगा ही। मेरी तरह निठल्ले लोग गाँव-भर में दस-पाँच ही तो बचे।’’
देवता सिंह की बात को ही विस्तार दिया माताजी ने, ‘‘आप तो दूरा-दरवाजा की बात करते हैं, घर की औरतें भी तो चली जाती हैं। अपने गाँव के चारों स्कूलों में कितनी देवीजी हैं ?’’
‘‘मैंने गिनती कर रखी है, दादी। प्राइमरी स्कूल में चार, मिडिल स्कूल में पाँच और कन्यापाठ शाला में तो सात-की-सात देवियाँ हैं ही। हाई-स्कूल में भी अब चार हो गईं। और इसके अलावा अपने गाँव की चारों सीमाओं पर बसे गाँवों में भी तो अपने गाँव की औरतें मास्टरनी हैं। कुल मिलाकर पचास मास्टरनी हैं अपने गाँव की।’’
‘‘दुर ! तू भी झूठ ही बोलने लगा। पढ़ा-लिखा है न।’’ दादी ने प्यार भरी झिड़की दी विजय को।
‘‘नहीं, भौजी ! आप समझी नहीं। अपने गाँव की बेटियाँ जो दूसरे गाँवों में ब्याही हैं, और वहाँ जाकर मास्टरनी बनीं, उनके् नाम भी जोड़ लिये विजय ने। देवता सिंह से अपने अनुसार गिनती कर ली।
‘‘तब तो और भी झूठ है। बाप रे ! बीस-पच्चीस बरस में तो न जाने कितनी लड़कियाँ ट्रेनिंग करके ससुराल गईं। लेकिन एक बात है। ट्रेनिंग की हुई लड़की की शादी का झमेला नहीं होता। दूसरे गाँव के लोग भी तो मास्टरनी बहू चाहते हैं। तिलक-दहेज ज्यादा नहीं मिला तो भी क्या, मास्टरनी तो मिलती है।’’
भाभी का समर्थन किया देवता सिंह ने, ‘‘क्यों नहीं ! बुढ़ापे तक अपने खूँटे से कामधेनु गाय बांधे रखते हैं।’’
माताजी देवता सिंह की उपमा की तह तक न जाकर बोल पड़ीं, ‘‘कुछ भी कहिए, मुझे औरतों का गाँव-घर से पैर बाहर निकालना अच्छा नहीं लगता। मास्टरनी अब तो ससुर–भैंसुर के आगे पैर निकालकर चलती ही थीं, अब तो अस्पताल में भी जाकर पता नहीं क्या काम करने लगी हैं औरतें !’’
‘‘मिडवाइफ और नर्स हो रही हैं, दादी। बच्चा पैदा करवाती हैं और रोगी की सेवा-शुश्रूषा करती हैं। अच्छी तनख्वाह मिलती है और ऊपर से इनाम, बख्शीश भी।’’
‘‘मारो झाड़ू से। ये सब काम कहीं भले घर की बहू-बेटियों का है ! छिह ! छिह !! पैसा की खातिर मर्द लोग क्या-क्या करवाने लगे अपनी औरतों से; मुझे अच्छा नहीं लगता। मर्द ही नाच नचाते हैं।’’
थोड़ी देर चुप्पी बनी रही। माताजी ने फिर कहा, ‘‘बबुआ नहीं आए ! बड़ी देर हो गई !’’
‘‘दादी, आप अच्छा-खासा भाषण दे लेती हैं। अगली बार चुनाव में आपको विरोधी दल का उम्मीदवार बनाया जा सकता है।’’ विजय ने हँसते हुए कहा।
पर जब तक माताजी विजय की बात समझतीं और चुनाव पर अपना मत व्यक्त करतीं, उनके पुत्र रामजीवन सिंह आ गए। माताजी ने राहत की साँस ली।
रामजीवन सिंह ने विजय की आधी बात सुन ली थी। पूछा, ‘‘किसे उम्मीदवार बना रहे हो ?’’
‘‘भौजी को ! देवता सिंह ने कहा।
दरवाजे पर बैठे सब लोगों की मिली-जुली हँसी गूँज उठी है।
विजय हँसते हुए बोला, ‘‘चाचा, दादी विरोधी दल के नेता के नाते अच्छा भाषण दे सकती हैं। अभी एक घंटा से समाचार पत्र, पढ़ाई लिखाई, नौकरी-चाकरी के विरोध में बोल रही थीं।’’
पुनः हँसी की फुहार बरसने के पहले ही रामजीवन सिंह की मुद्रा देख थम गई।
देवता सिंह ने पूछा, ‘‘क्या समाचार है बबुआ ?’’
‘‘बहुत खराब !’’ रामजीवन सिंह के दो शब्द उसके मन की गहन चिंता से सराबोर थे।
‘‘क्या हुआ ?’’ माताजी ने उत्कंठा जताई, ‘‘अखबार पढ़कर सुना तो ! देश-दुनिया में सब ठीक है न ?’’
समाचार सुनने की उनकी उत्सुकता ने सबको विस्मित कर दिया।
‘‘नहीं, माँ ! ठीक-ठाक कैसे होगा ! पंजाब की समस्या गहराती जा रही है। कल आतंकवादियों ने एक बस से दस लोगों को खींचकर मारा है। उनमें आठ तो बिहारी मजदूर थे।’’
खबर सुनते-सुनाते रामजीवन सिंह का स्वर भारी हो उठा। स्थिति की गंभीरता ने सबको अपने में लपेट लिया।
चुप्पी भंग की विजय ने, ‘‘चाचा, मरनेवालों के नाम भी लिखे हैं ?’’
जवाब में रामजीवन सिंह ने विजय की ओर अखबार बढ़ा दिया।
समाचारपत्र पढ़ने की बात आई तब सबके सब लालटेन की खोज करने लगे। रामजीवन सिंह झल्लाए, ‘‘अब तक लालटेन भी नहीं जलाई ?’’
‘‘अरी सुष्मी ! जरा लालटेन जला के लाना।’’ दादी ने पोती को आज्ञा देकर कहा, ‘‘अरे बेटा ! ऐसी टहटही इँजोरिया (साफ चाँदनी) में साँझे से क्या लालटेन जलाएँ। किरासन तेल भी तो नहीं मिलता। किना महँगा है ! कु्आँ-पोखर से तो नहीं खिंचता है न तेल। मोल लेना पड़ता है। बज्र पड़े बिजली की लाइन में ! नाम के लिए है। कभी-कभी भुक-भुक कर जाती है।’’
सब जानते हैं कि माँ के आगे रामजीवन की एक नहीं चलती। उनकी खेती-बाड़ी, माल-मवेशी और घर-द्वार—सबकुछ तो माँ ही सँभालती हैं। घर की मालिक और मालकिन वही आई हैं रामजीवन सिंह को अपनी मास्टरी और सामाजिक कार्यों से फुरसत ही कहाँ मिलती है ! उनकी पत्नी को इस घर में बहू बनकर आए तीस बरस बीत गए। अब अपनी भी बहू आनेवाली है; पर अब तक सास का हुक्म बजाती आई है, मालकिन नहीं बन पाई।
विजय अन्दर गया और लालटेन ले आया। समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ पर ही लिखा समाचार सुन श्रोताओं के दिल दहल गए। सबके सब चुप।
‘‘और जाएँ पंजाब। काटें गेहूँ। खाएँ मालपुआ। समझा-बुझा के कहे—रे, पंजाब न जा। अपने गाँव की धरती को जोतो, कोड़ों; जो रूखा-सूखा मिले, खा—पीकर गुजर करो। बाल-बच्चे के साथ रहोगे। कौन माने मेरी बात !’’ रामजीवन सिंह की माँ अपने गाँव के तमाम मुसहर, धोबी, चमार—जो पिछले कई वर्षों से पंजाब जाते रहे हैं, उनपर झुँझला उठीं। उनकी झल्लाहट में अपने ग्रामीण मजदूरों के लिए अपनेपन में सना क्रोध था, मरनेवालों के प्रति वेदना थी।
‘‘भौजी, पंजाब न जाते तो रेडियो कैसे बजाते ? मुसहरनी सब छींट की साड़ी कैसे पहनतीं ? अरे, बाप रे ! कैसी-कैसी लहकदार साड़ियाँ पहनकर गाँव भर में घूमती हैं ! अब तो हम लोगों से भी कोई लाज, न शरम।’’ देवता सिंह ने मुसहरनियों के प्रति अपने मन का गुबार निकाला।
अगर रामजीवन सिंह पंजाब की स्थिति की गंभीरता की ओर ध्यान नहीं खींचते तो सबके सब अपने गाँव के मजदूरों के ऊपर ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रह जाते और उनकी माताजी की सभाध्यक्षता बनी रहती।
‘‘भई, गाँव में काम नहीं मिलता तो पंजाब, असम या कलकत्ता क्यों नहीं जाएँ ? आखिर पेट तो पालना ही है। गाँव में भूखों मरने से अच्छा है, कहीं जाकर रोटी कमाना। कुछ ही वर्षों से तो पंजाब जाने लगे हैं। बिहार के मजदूर तो पहले असम, कलकत्ता जाते रहे। असमियों ने हो-हल्ला मचाया तो अब उन्होंने अपने पैरों की दिशा पूरब से उत्तर-पश्चिम कर ली। अब पंजाबवालों ने मारना शुरू किया है—
आगे-आगे देखो, होता है क्या ?’’ रामजीवन सिंह के पीड़त मन के बोल थे।
मरनो भलो विदेश में जहाँ न अपनो कोय
माटी खाय जनावराँ महामहोत्सव होय ।।
माटी खाय जनावराँ महामहोत्सव होय ।।
देवतासिंह ने मास्टर साहब की आह की व्याख्या की उन्होंने रामजीवन सिंह के
मन को हलका करना चाहा था। आगे बोले, ‘‘आप ही तो कहते
हैं कि विदेश में भी बिहारी मजदूर बसे हैं।’’
‘‘कोई आज की बात तो है नहीं। सैकड़ों वर्षों से बिहार के मजदूरों को भारत से बाहर फिजी, गायना, सूरीनाम और मॉरीशस में ले जाया गया। उन्होंने वहाँ मजदूरी की और वहीं बस गए। अब वहाँ वे मजदूर नहीं रहे। खूब पैसेवाले हो गए हैं। वहाँ की राजनीति में भी सक्रिय हैं। अब तो उनके बाल-बच्चे बिहार में आकर अपने गाँव तलाशने लगे हैं। परंतु आज तो विदेश क्या, देश में भी बिहारी मजदूरों की जान सुरक्षित नहीं है। पंजाब जाकर मेहनत करते हैं। वहाँ से भी भागने लगेंगे। परंतु उनकी समस्या से बढ़कर भारी समस्या तो देश की है। पंजाब के विभाजन की समस्या, खालिस्तान की माँग करनेवालों द्वारा पैदा की गई समस्या। न जाने इस देश के भाग्य में कितने विभाजन लिखे हैं !’’
विजय ने उत्सुकता जताई, ‘‘चाचा, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ये पंजाबी लोग चाहते क्या हैं ?’’
‘‘कितनी बार तुम लोगों को बताया कि सभी पंजाबी ऐसा नहीं चाहते ! पंजाब में रहनेवाले लोगों का एक वर्ग ‘सिख’ और दूसरा वर्ग ‘मोना’ कहलाता है। वैसे दोनों हैं तो हिंदू ही, परंतु सरदार दाढ़ी-मूँछ बढ़ाकर पगड़ी बाँधकर रहते हैं और मोना लोग हमारी तरह। सामाजिक दृष्टि से दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। आपस में शादी-ब्याह भी होते रहे हैं। परंतु कुछ बहके हुए सिख खालिस्तान की माँग करने लगे और उन्होंने अपनी माँग के लिए उत्पात मचाना प्रारम्भ कर दिया है। इन्हें ही उग्रवादी, आतंकवादी या खाड़कू कहा जा रहा है।’’
‘‘तो क्या इस खून-खराबे में पंजाबी लोग भी मारे जा रहे हैं, या सिर्फ बिहारी ?’’ किसी दूसरे नौजवान ने अपनी उत्सुकता जताई।
सर्गिक सौंदर्य पर आतंकवादी गतिविधियों की पड़ी कलुषित छाया के दर्द और दंश को रेखांकित कर भारतीय प्रांतों की परस्पर निर्भरता को दरशाया गया है।
‘‘कोई आज की बात तो है नहीं। सैकड़ों वर्षों से बिहार के मजदूरों को भारत से बाहर फिजी, गायना, सूरीनाम और मॉरीशस में ले जाया गया। उन्होंने वहाँ मजदूरी की और वहीं बस गए। अब वहाँ वे मजदूर नहीं रहे। खूब पैसेवाले हो गए हैं। वहाँ की राजनीति में भी सक्रिय हैं। अब तो उनके बाल-बच्चे बिहार में आकर अपने गाँव तलाशने लगे हैं। परंतु आज तो विदेश क्या, देश में भी बिहारी मजदूरों की जान सुरक्षित नहीं है। पंजाब जाकर मेहनत करते हैं। वहाँ से भी भागने लगेंगे। परंतु उनकी समस्या से बढ़कर भारी समस्या तो देश की है। पंजाब के विभाजन की समस्या, खालिस्तान की माँग करनेवालों द्वारा पैदा की गई समस्या। न जाने इस देश के भाग्य में कितने विभाजन लिखे हैं !’’
विजय ने उत्सुकता जताई, ‘‘चाचा, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ये पंजाबी लोग चाहते क्या हैं ?’’
‘‘कितनी बार तुम लोगों को बताया कि सभी पंजाबी ऐसा नहीं चाहते ! पंजाब में रहनेवाले लोगों का एक वर्ग ‘सिख’ और दूसरा वर्ग ‘मोना’ कहलाता है। वैसे दोनों हैं तो हिंदू ही, परंतु सरदार दाढ़ी-मूँछ बढ़ाकर पगड़ी बाँधकर रहते हैं और मोना लोग हमारी तरह। सामाजिक दृष्टि से दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। आपस में शादी-ब्याह भी होते रहे हैं। परंतु कुछ बहके हुए सिख खालिस्तान की माँग करने लगे और उन्होंने अपनी माँग के लिए उत्पात मचाना प्रारम्भ कर दिया है। इन्हें ही उग्रवादी, आतंकवादी या खाड़कू कहा जा रहा है।’’
‘‘तो क्या इस खून-खराबे में पंजाबी लोग भी मारे जा रहे हैं, या सिर्फ बिहारी ?’’ किसी दूसरे नौजवान ने अपनी उत्सुकता जताई।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book