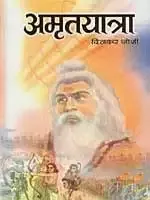|
पौराणिक >> अमृतयात्रा अमृतयात्रादिनकर जोशी
|
213 पाठक हैं |
||||||
एक कालजयी व ह्रदयस्पर्शी उपन्यास...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
तत्त्कालीन आर्यावर्त्त के दुर्दम्य योद्धा और हस्तिनापुर के प्रतिष्ठित
आचार्य द्रोण के जीवन पर आधारित एक मार्मिक उपन्यास। द्रोणाचार्य ने अपने
जीवन में तमाम विडंबनाओं और त्रासदियों को भोगा। उनकी जीवन मान-अपमान,
न्याय-अन्याय, धर्म-अधर्म के मध्य उलझता-सुलझता रहा। उनकी जीवनयात्रा
अमृतयात्रा ही तो है। एक कालजयी व ह्रदयस्पर्शी उपन्यास जो अत्यंत व पठनीय
है।
अमृतयात्रा
श्री केळेकर कोंकणी भाषा के एक वरिष्ठ
साहित्यकार हैं।
केंद्रीय साहित्य अकादमी, दिल्ली में कोंकणी भाषा के प्रतिनिधि के रूप में
उन्होंने बहुत समय तक सेवा की है। उन्होंने ‘महाभारत’
का गहन
अध्ययन किया है और कोंकणी भाषा में ‘महाभारत’ के
संदर्भ का
तीन भागों में एक वृहद् ग्रंथ लिखा है। गोवा में एक ऊँची और एकांत पहाड़ी
पर स्थित उनके निवास-स्थान पर बैठकर हम बात कर रहे थे।
‘महाभारत’ में हम दोनों की समान रुचि होने के कारण
हमारी
चर्चा का केंद्रबिंदु ‘महाभारत’ बन गया। बातचीत के
दौरान
उन्होंने मुझसे पूछा, ‘‘धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र
था,
जिसका जन्म ही द्रोण के वध के लिए हुआ था। फिर क्या कारण था कि द्रोण ने
अपने उस भावी हत्यारे को धनुर्विद्या की शिक्षा दी, उसे शिष्य-रूप में
स्वीकार किया ?’
श्री केळेकर का यह प्रश्न सुनकर मुझे ‘श्रीमद्भगवतद्गीता’ के प्रथम अध्याय ‘अर्जुनविषादयोग’ का स्मरण हो आया। युद्ध के आरंभ में ही दुर्योधन द्रोण से कहता है, ‘‘आचार्य ! हमारी सेना पितामह भीष्म से रक्षित है। शत्रु-सेना आपको शिष्य धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में सन्नद्ध खड़ी है।’’
धृष्टद्युम्न द्रोण का शिष्य किस प्रकार बना होगा ? पहले तो लगा कि उस युग के सम्मुख उपस्थिति हुआ होगा और द्रोण ने उसे स्वीकार कर लिया होगा। परंतु ‘महाभारत’ के आदिपर्व में जो स्पष्ट उल्लेख है, उससे यह भावना निर्मूल सिद्ध हो जाती है। द्रोण स्वयं ही द्रुपद के इस पुत्र को अपने पास लाए थे और धनुर्विद्या का अभ्यास कराया था। द्रुपद और द्रोण के बीच का वैमनस्य सर्वविदित था। द्रुपद ने अपनी पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए ही यज्ञदेवता से पुत्र प्राप्त किया था। यह बात भी किसी से छिपी नहीं थी। यह जानते हुए भी द्रोण ने अपने ही वध के लिए उत्पन्न शत्रु को अपना शिष्य क्यों बनाया ?
‘महाभारत’ में द्रोण के विषय में जो भी उल्लेख प्राप्त हुआ, उन सबको एकत्र करके अलग किया तो पूर्वोक्त एक प्रश्न का उत्तर मिलने के बजाय द्रोण के जीवन से संबंधित कई अन्य आनुषंगिक प्रश्न भी प्राप्त हुए। द्रोण जीवन के आरंभ में अकिंचन और दरिद्र ब्राह्मण थे, यह सही है। परंतु वे महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। ज्ञान और त्याग के प्रतीक-स्वरूप वेद और कमंडलु उनकी ध्वजा पर चित्रित थे। द्रव्य-लालसा से वे आचार्य परशुराम के पास गए थे और यही लालसा लेकर वे द्रुपद के पास भी गए थे, यह भी सही है; किंतु हस्तिनापुर में तो द्रुपद के प्रति अपनी प्रतिशोध-भावना की तृप्ति के लिए ही रहे थे। पर प्रश्न है, इस तरह द्रव्य-लालसा और प्रतिरोध-भावना से सभर होते हुए भी द्रोण ने धृष्टद्युम्न को एक उत्तम धनुर्धर क्यों बनाया ?
द्रोण ने द्रव्य भी प्राप्त किया और उनकी प्रतिशोध-भावना भी तृप्त हो गई। इसके बाद तो हस्तिनापुर में उनका स्थान पितामह भीष्म के बाद दूसरे क्रम पर हो गया। द्रोपदी वस्त्र-हरण के समय पितामह भीष्म की भूमिका समझ में न आनेवाली बात है। किंतु भीष्म तो कुरुकुल के ही एक प्रमुख व्यक्ति थे, ऊपर से प्रतिज्ञाबद्ध भी। द्यूतसभा को तो कुरुकुल का एक पारिवारिक आयोजन ही कहा जाएगा। इस प्रसंग में वे मात्र मौन ही नहीं रहते, बल्कि द्रोपदी के प्रश्नों के उत्तर देने से वर्तमान राजनेताओं जैसा कतराने का स्पष्ट प्रयास भी करते हैं। भीष्म ने ऐसा क्यों किया होगा ? और भीष्म ने परिवार में सबसे वयोवृद्ध होने के कारण ऐसा किया भी हो तो राजसभा में दूसरे क्रम पर स्थित महर्षि भरद्वाज के पुत्र क्यों मौन रहे ? जबकि अब उनका कोई उद्देश्य पूर्ण होना शेष नहीं रह गया था ! किन अदृश्य कारणों ने उन्हें इस अधर्म का मूक समर्थन करने के लिए प्रेरित किया होगा ? वे हस्तिनापुर के एक वेतनभोगी शिक्षक थे, मात्र इसलिए उन्होंने इस अधर्म को अनदेखा किया होगा, क्या यह संभव है ?
प्रश्नों का क्रम और लंबा चलता है।
द्रोपदी-स्वयंवर उस समय की एक स्वीकृत प्रथा का ही अंग था, क्या यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है ? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एक अन्य संभावना की ओर संकेत करते हैं। समग्र महाभारत ग्रंथ में कृष्ण-द्रौपदी का सख्यभाव अद्भुत और आह्वादक है। इस तरह के सख्यभाव के विकसित होने की घटना महर्षि व्यास ने हमसे नहीं कही है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार, कृष्ण-द्रौपदी का प्रथम मिलन तो उस समय हुआ, जब द्रोपदी पांडवों की पत्नी बनकर पांचाल नगरी के सीमांत पर स्थित एक कुम्हार के घर आई थी, जहाँ पांडव तापस के रूप में अज्ञातवास में थे। उस समय भी दोनों के बीच कोई वार्त्तालाप नहीं होता। सख्यभाव दरशानेवाली पहली बात चीत तो वन पर्व में होती है, जब राज्य गँवाकर पांडव अरण्यवास पूरा कर रहे होते हैं। ऐसे इस सख्यभाव का विकास कब और कैसे हुआ होगा ? द्रुपद और कृष्ण के बीच कोई विशिष्ट घनिष्टता संबंध रहा होगा ? स्मरण रहे, श्रीकृष्ण तो एक अत्यंत उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ थे ही ! कृष्ण की आर्ष राजनीति को स्पष्ट करनेवाले प्रसंग ‘महाभारत’ में देखे जा सकते हैं।
तेरहवें वर्ष का अरण्यवास पांडवों को गुप्त वेश में करना था। विराट नगरी में कीचक-वध की घटना के बाद दुर्योधन विराट के हस्तिनापुर का कोई वैर नहीं। तेरहवें वर्ष में पांडवों के विषय में दुर्योधन कोई सूचना प्राप्त नहीं कर पाता, जिससे वह यही निष्कर्ष निकालता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। फिर भी विराट की गायें अपहृत करने जैसा निकृष्ट आयोजन करने में वह संकोच नहीं करता, दुर्योधन के चरित्र को हम ध्यान में रखें तो संभवतः यह सुसंगत लगे, किंतु भीष्म और द्रोण जैसों ने यह प्रस्ताव क्यों स्वीकार कर लिया, यह समझ के बाहर है। गायों को हरने का कार्य तो मात्र लूटपाट का ही कृत्य था न ! इसमें न तो वीरता थी, न कोई सिद्धांत या शौर्य ! यही नहीं, इस निकृष्ट कार्य में भी भीष्म और द्रोण जैसे अपराजेय योद्धा अकेले अर्जुन के हाथों पराजित हुए। यह कैसे संभव हुआ होगा ?
कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में द्रोणाचार्य ने चक्र व्यूह की रचना की। उस समय द्रोण स्वयं सेनापति थे और वे यह भली-भाँति जानते थे कि चक्र व्यूह का भेदन एकमात्र अर्जुन ही कर सकते थे। अर्जुन को अन्य दिशा में उलझाकर चक्र व्यूह का भेदन रचना करके, अधर्म का आश्रय लेकर द्रोण ने अभिमन्यु की हत्या जैसे कुकृत्य में सहयोग क्यों किया ? चक्र व्यूह का आयोजन करके अर्जुन को युद्ध करने का उन्होंने अवसर दिया होता तो यह धर्माचरण माना जाता; किंतु यह अधर्माचरण उन्होंने क्यों किया ?
महाभारत के पंद्रहवें दिन ‘ अश्वत्थामा हतो’ सुनकर सेना पति द्रोण ने शस्त्र-त्याग किया था। शस्त्रहीन द्रोण पर प्रहार करके स्वयं उनके ही शिष्य और पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न ने उनका शिरश्छेद कर दिया, ऐसा उल्लेख महाभारत में है। धृष्टद्युम्न के आचरण में इसके पूर्व किसी प्रकार की नीचता या हीनता का प्रमाण हमें नहीं मिलता। जिस कृत्य से विचलित होकर स्वयं अर्जुन धृष्टद्युम्न पर प्रहार करने को उद्यत हो गए हों, आर्यावर्त की इस घटना का विश्लेषण कैसे किया जा सकता है ? धृष्टद्युम्न ने ऐसी हीनता क्या मात्र युद्ध के आवेग में ही की होगी ?
इन सभी प्रश्नों के उत्तर महाभारत में ‘इति सिद्धम्’ स्वरूप में नहीं मिलते। जहाँ रहस्योद्घाटन नहीं हो पाता वहां संदर्भों, पात्रों तथा घटनाओं की संवादिता अक्षुण्ण रखते हुए तर्कसंगत अनुमानों का आश्रय लेना पड़ता है।‘अमृतयात्रा’ ऐसा की एक आयास है। इसमें कुछ ऐसे अनुमानों का भी आश्रय लिया गया है जिन्हें स्थूल रूप में वेदव्यास ने अक्षरबद्ध नहीं किया है, किंतु मनोविज्ञान और तर्क की दृष्टि से वे संभावनाओं और अनुमानों का आश्रय लेने का अधिकार मुझे है, उनका कहीं-कहीं उपयोग मैंने अवश्य किया है, यह स्पष्ट कर दूँ।
नहीं तो महाभारत एक ऐसा महोदधि है, जिसकी हर तरंग में नए रहस्य और सौंदर्य प्रकट होते हैं। इन रहस्यों और सौंदर्यों का पार पाना संभव नहीं। हम तो मोनालिसा की स्मित भी नहीं पहचान सकते तो व्यास के कृतित्व को समझ पाना हमारे सामर्थ्य में कहाँ !
प्रश्नों के पार के प्रदेश में यात्रा करने के लिए यह निमंत्रण है। महाभारत के कथानकों से सुपरिचित सहयात्री इसमें अपेक्षित तो हैं ही, पर जो उनके अल्पपरिचित या अपरिचित हैं, उन्हें भी यह यात्रा उस प्रदेश में ले जाए तो मेरा यह आयास सफल समझा जाएगा।
श्री केळेकर का यह प्रश्न सुनकर मुझे ‘श्रीमद्भगवतद्गीता’ के प्रथम अध्याय ‘अर्जुनविषादयोग’ का स्मरण हो आया। युद्ध के आरंभ में ही दुर्योधन द्रोण से कहता है, ‘‘आचार्य ! हमारी सेना पितामह भीष्म से रक्षित है। शत्रु-सेना आपको शिष्य धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में सन्नद्ध खड़ी है।’’
धृष्टद्युम्न द्रोण का शिष्य किस प्रकार बना होगा ? पहले तो लगा कि उस युग के सम्मुख उपस्थिति हुआ होगा और द्रोण ने उसे स्वीकार कर लिया होगा। परंतु ‘महाभारत’ के आदिपर्व में जो स्पष्ट उल्लेख है, उससे यह भावना निर्मूल सिद्ध हो जाती है। द्रोण स्वयं ही द्रुपद के इस पुत्र को अपने पास लाए थे और धनुर्विद्या का अभ्यास कराया था। द्रुपद और द्रोण के बीच का वैमनस्य सर्वविदित था। द्रुपद ने अपनी पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए ही यज्ञदेवता से पुत्र प्राप्त किया था। यह बात भी किसी से छिपी नहीं थी। यह जानते हुए भी द्रोण ने अपने ही वध के लिए उत्पन्न शत्रु को अपना शिष्य क्यों बनाया ?
‘महाभारत’ में द्रोण के विषय में जो भी उल्लेख प्राप्त हुआ, उन सबको एकत्र करके अलग किया तो पूर्वोक्त एक प्रश्न का उत्तर मिलने के बजाय द्रोण के जीवन से संबंधित कई अन्य आनुषंगिक प्रश्न भी प्राप्त हुए। द्रोण जीवन के आरंभ में अकिंचन और दरिद्र ब्राह्मण थे, यह सही है। परंतु वे महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। ज्ञान और त्याग के प्रतीक-स्वरूप वेद और कमंडलु उनकी ध्वजा पर चित्रित थे। द्रव्य-लालसा से वे आचार्य परशुराम के पास गए थे और यही लालसा लेकर वे द्रुपद के पास भी गए थे, यह भी सही है; किंतु हस्तिनापुर में तो द्रुपद के प्रति अपनी प्रतिशोध-भावना की तृप्ति के लिए ही रहे थे। पर प्रश्न है, इस तरह द्रव्य-लालसा और प्रतिरोध-भावना से सभर होते हुए भी द्रोण ने धृष्टद्युम्न को एक उत्तम धनुर्धर क्यों बनाया ?
द्रोण ने द्रव्य भी प्राप्त किया और उनकी प्रतिशोध-भावना भी तृप्त हो गई। इसके बाद तो हस्तिनापुर में उनका स्थान पितामह भीष्म के बाद दूसरे क्रम पर हो गया। द्रोपदी वस्त्र-हरण के समय पितामह भीष्म की भूमिका समझ में न आनेवाली बात है। किंतु भीष्म तो कुरुकुल के ही एक प्रमुख व्यक्ति थे, ऊपर से प्रतिज्ञाबद्ध भी। द्यूतसभा को तो कुरुकुल का एक पारिवारिक आयोजन ही कहा जाएगा। इस प्रसंग में वे मात्र मौन ही नहीं रहते, बल्कि द्रोपदी के प्रश्नों के उत्तर देने से वर्तमान राजनेताओं जैसा कतराने का स्पष्ट प्रयास भी करते हैं। भीष्म ने ऐसा क्यों किया होगा ? और भीष्म ने परिवार में सबसे वयोवृद्ध होने के कारण ऐसा किया भी हो तो राजसभा में दूसरे क्रम पर स्थित महर्षि भरद्वाज के पुत्र क्यों मौन रहे ? जबकि अब उनका कोई उद्देश्य पूर्ण होना शेष नहीं रह गया था ! किन अदृश्य कारणों ने उन्हें इस अधर्म का मूक समर्थन करने के लिए प्रेरित किया होगा ? वे हस्तिनापुर के एक वेतनभोगी शिक्षक थे, मात्र इसलिए उन्होंने इस अधर्म को अनदेखा किया होगा, क्या यह संभव है ?
प्रश्नों का क्रम और लंबा चलता है।
द्रोपदी-स्वयंवर उस समय की एक स्वीकृत प्रथा का ही अंग था, क्या यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है ? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एक अन्य संभावना की ओर संकेत करते हैं। समग्र महाभारत ग्रंथ में कृष्ण-द्रौपदी का सख्यभाव अद्भुत और आह्वादक है। इस तरह के सख्यभाव के विकसित होने की घटना महर्षि व्यास ने हमसे नहीं कही है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार, कृष्ण-द्रौपदी का प्रथम मिलन तो उस समय हुआ, जब द्रोपदी पांडवों की पत्नी बनकर पांचाल नगरी के सीमांत पर स्थित एक कुम्हार के घर आई थी, जहाँ पांडव तापस के रूप में अज्ञातवास में थे। उस समय भी दोनों के बीच कोई वार्त्तालाप नहीं होता। सख्यभाव दरशानेवाली पहली बात चीत तो वन पर्व में होती है, जब राज्य गँवाकर पांडव अरण्यवास पूरा कर रहे होते हैं। ऐसे इस सख्यभाव का विकास कब और कैसे हुआ होगा ? द्रुपद और कृष्ण के बीच कोई विशिष्ट घनिष्टता संबंध रहा होगा ? स्मरण रहे, श्रीकृष्ण तो एक अत्यंत उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ थे ही ! कृष्ण की आर्ष राजनीति को स्पष्ट करनेवाले प्रसंग ‘महाभारत’ में देखे जा सकते हैं।
तेरहवें वर्ष का अरण्यवास पांडवों को गुप्त वेश में करना था। विराट नगरी में कीचक-वध की घटना के बाद दुर्योधन विराट के हस्तिनापुर का कोई वैर नहीं। तेरहवें वर्ष में पांडवों के विषय में दुर्योधन कोई सूचना प्राप्त नहीं कर पाता, जिससे वह यही निष्कर्ष निकालता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। फिर भी विराट की गायें अपहृत करने जैसा निकृष्ट आयोजन करने में वह संकोच नहीं करता, दुर्योधन के चरित्र को हम ध्यान में रखें तो संभवतः यह सुसंगत लगे, किंतु भीष्म और द्रोण जैसों ने यह प्रस्ताव क्यों स्वीकार कर लिया, यह समझ के बाहर है। गायों को हरने का कार्य तो मात्र लूटपाट का ही कृत्य था न ! इसमें न तो वीरता थी, न कोई सिद्धांत या शौर्य ! यही नहीं, इस निकृष्ट कार्य में भी भीष्म और द्रोण जैसे अपराजेय योद्धा अकेले अर्जुन के हाथों पराजित हुए। यह कैसे संभव हुआ होगा ?
कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में द्रोणाचार्य ने चक्र व्यूह की रचना की। उस समय द्रोण स्वयं सेनापति थे और वे यह भली-भाँति जानते थे कि चक्र व्यूह का भेदन एकमात्र अर्जुन ही कर सकते थे। अर्जुन को अन्य दिशा में उलझाकर चक्र व्यूह का भेदन रचना करके, अधर्म का आश्रय लेकर द्रोण ने अभिमन्यु की हत्या जैसे कुकृत्य में सहयोग क्यों किया ? चक्र व्यूह का आयोजन करके अर्जुन को युद्ध करने का उन्होंने अवसर दिया होता तो यह धर्माचरण माना जाता; किंतु यह अधर्माचरण उन्होंने क्यों किया ?
महाभारत के पंद्रहवें दिन ‘ अश्वत्थामा हतो’ सुनकर सेना पति द्रोण ने शस्त्र-त्याग किया था। शस्त्रहीन द्रोण पर प्रहार करके स्वयं उनके ही शिष्य और पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न ने उनका शिरश्छेद कर दिया, ऐसा उल्लेख महाभारत में है। धृष्टद्युम्न के आचरण में इसके पूर्व किसी प्रकार की नीचता या हीनता का प्रमाण हमें नहीं मिलता। जिस कृत्य से विचलित होकर स्वयं अर्जुन धृष्टद्युम्न पर प्रहार करने को उद्यत हो गए हों, आर्यावर्त की इस घटना का विश्लेषण कैसे किया जा सकता है ? धृष्टद्युम्न ने ऐसी हीनता क्या मात्र युद्ध के आवेग में ही की होगी ?
इन सभी प्रश्नों के उत्तर महाभारत में ‘इति सिद्धम्’ स्वरूप में नहीं मिलते। जहाँ रहस्योद्घाटन नहीं हो पाता वहां संदर्भों, पात्रों तथा घटनाओं की संवादिता अक्षुण्ण रखते हुए तर्कसंगत अनुमानों का आश्रय लेना पड़ता है।‘अमृतयात्रा’ ऐसा की एक आयास है। इसमें कुछ ऐसे अनुमानों का भी आश्रय लिया गया है जिन्हें स्थूल रूप में वेदव्यास ने अक्षरबद्ध नहीं किया है, किंतु मनोविज्ञान और तर्क की दृष्टि से वे संभावनाओं और अनुमानों का आश्रय लेने का अधिकार मुझे है, उनका कहीं-कहीं उपयोग मैंने अवश्य किया है, यह स्पष्ट कर दूँ।
नहीं तो महाभारत एक ऐसा महोदधि है, जिसकी हर तरंग में नए रहस्य और सौंदर्य प्रकट होते हैं। इन रहस्यों और सौंदर्यों का पार पाना संभव नहीं। हम तो मोनालिसा की स्मित भी नहीं पहचान सकते तो व्यास के कृतित्व को समझ पाना हमारे सामर्थ्य में कहाँ !
प्रश्नों के पार के प्रदेश में यात्रा करने के लिए यह निमंत्रण है। महाभारत के कथानकों से सुपरिचित सहयात्री इसमें अपेक्षित तो हैं ही, पर जो उनके अल्पपरिचित या अपरिचित हैं, उन्हें भी यह यात्रा उस प्रदेश में ले जाए तो मेरा यह आयास सफल समझा जाएगा।
-दिनकर जोशी
एक
हस्तिनापुर के राजमार्गों पर शीतल जल का
छिड़काव कर रहे
सेवक अभी-अभी अपने काम से निवृत्त हुए थे। प्राची का पीताभ वर्ण अब अदृश्य
हो गया था और नगर में फैली सूर्य की किरणों में अब किशोरावस्था प्रवेश कर
चुकी थी। गीली धरती की सोंधी महक हवा के साथ ऐसी कोमलता से लिपट गई थी कि
किसी को भी एक क्षण गहरी साँस लेने का मन हो जाए। प्राणवायु को परिप्लावित
कर दे, ऐसा एक अन्य तत्त्व भी वातावरण में आवर्तन रच रहा था। राजमार्गों
के दोनों ओर फैले आवास और दूर-दूर तक ध्वजाओं एवं गवाक्षों द्वारा अपने
अस्तित्व का बोध कराते राजपरिवार के महालयों के प्रांगण से प्रातः संध्या
की यज्ञवेदी की अग्नि-ज्वाला से प्रकट होती धूम रेखाओं में आहुति की
शुद्धि और पवित्रता हवा में मिलती जा रही थी। धरती की महक और आहुति की
पवित्रता के बीच हस्तिनापुर जैसे सूर्य किरणों के अंक में झूल रहा था।
नगर की पूर्व सीमा से प्रवेश करते ही कुछ कदम चलने के बाद एक सुंदर पगडंडी मुख्य मार्ग से फूट निकलती थी। इस पगडंडी पर एक ऐसा आवास दिखाई देता था, जिसे महालय कहें तो तपोवन लगे और तपो वन कहें तो उसके महालय होने की साक्षी देते तत्त्व उड़कर आँखों में गड़ने लगें। प्रांगण में ही लगे ध्वज में विचित्र-वेद ग्रंथों और कमंडलु के चित्र इस आवास में रहनेवालों के ज्ञान और त्याग के प्रतीक लग रहे थे। विशाल प्रांगण के ठीक मध्य में प्रज्वलित यज्ञवेदी के समीप ही एक विशाल चौकी पर दृष्टि पड़ते ही जिसके प्रभाव में आ जाए, ऐसा एक धनुष रखा हुआ था। यज्ञवेदी से निकलती धूम-रेखाओं के साथ ही इस धनुष का पूजन भी अभी-अभी होने का प्रमाण देते पुष्प उसके ऊपर फैले हुए थे।
यह आवास आचार्य द्रोण का था।
प्रातः संध्या और धनुष-पूजन से निवृत्त होकर आचार्य द्रोण अपने नित्य के आसन की ओर घूमे। यज्ञवेदी से कुछ ही दूर एक विशाल वृक्ष के नीचे काष्ट की एक ऊँची चौकी पर व्याघ्र-चर्म बिछाकर पुत्र अश्वात्थामा पिता के आसनस्थ होने की प्रतीक्षा में खड़ा था। स्वाध्याय-कक्ष में बैठकर शिष्यगण प्रतिदिन प्रातः विद्याध्ययन में प्रवृत्त होते तो उस समय द्रोण प्रातः संध्या पूर्ण करते। सूर्य किरणों के पूरी तरह फैल जाने तक स्वाध्याय-कक्ष में वेदाध्ययन चलता रहता। वेदाध्ययन के अंत में शांति-पाठ होता और उसके बाद सभी शिष्य बाहर पटांगण में आकर शस्त्राभ्यास करते। कोई गज-विद्या, कोई रथ-विद्या कोई गदा-युद्ध तो कोई खड्ग-युद्ध में निपुणता प्राप्त करने के लिए आचार्य के सम्मुख उपस्थित होता। उन सबको आचार्य द्रोण पुत्रवत् स्नेह देकर विद्याभ्यास कराते। इस शिष्य समूह में कई राजपुत्र थे तो कई ऐसे ब्राह्मण-पुत्र भी थे, जिन्होंने स्वेच्छया क्षात्र धर्म स्वीकार कर लिया था। कुरुवंश के आचार्य पद पर स्थापित होने के बाद द्रोणाचार्य की प्रतिष्ठा आर्यावर्त में बहुत बढ़ गई थी। तिस पर उनके पट्ट शिष्य अर्जुन के नेतृत्व में कौरवों और पांडवों ने मिलकर पांचाल-नरेश द्रुपद का जिस तरह पराभव किया था, उसकी कथा तो उत्तरापथ में एक किंवदंती ही बन गई थी।
धीमे, पर दृढ़ से द्रोण अपने व्याघ्र-चर्म बिछे आसन की ओर चले तो आसन के समीप तनकर खड़े अश्वत्थामा ने सहज ही अपना मस्तक किंचित् झुका दिया। द्रोण आसनस्थ हुए, वात्सल्यपूरित दृष्टि से पुत्र की ओर देखा। होंठ फड़काकर कोई मंत्रोच्चार किया और आँखें मूँद लीं।
‘‘तात !’’ अश्वत्थामा का स्वर नीरव शांति के बीच प्रकट हुआ।
द्रोण ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि से प्रश्न परिलक्षित था। द्रोण के आसनस्थ होने के पश्चात् अश्वत्थाना प्रतिदिन स्वाध्याय-कक्ष में लौट जाते थे। आज उसका इस तरह खड़ा रह जाना असामान्य था। आचार्य ने पुत्र पर दृष्टि स्थिर की। अश्वत्थामा की ताम्रवर्णी काया से मानो शक्ति और उत्साह का सागर उमड़ रहा था।
‘‘तुम कुछ बोले, वत्स ?’’ द्रोण ने धीरे से पूछा।
‘‘पिताजी !’’ अश्वत्थामा बोले, ‘‘एक शंका का समाधान चाहता हूँ।’’
‘‘शंका ?’’ द्रोण उठकर हँस पड़े।
‘‘जी हाँ ! मेरे मन में एक प्रश्न सदैव अनुत्तरित रहा है।’’
‘‘प्रश्न का उद्गम-स्थल यदि गंगोत्तरी जैसा पवित्र हो तो प्रश्न तो सदैव उपनिषदों की पूर्व भूमिका रहे हैं, पुत्र !’’ द्रोणाचार्य के होंठों पर किंचित् हास्य खेल गया।
‘‘मेरा प्रश्न इस उच्च स्तर का है कि नहीं, मैं यह नहीं जानता, पिताजी ! आपका आदेश हो तो मन में घुमड़ रही अपनी समस्या मैं आपके समक्ष प्रकट करूँ।’’
‘‘वत्स !’’ थोड़ा रुककर अपने नेत्र संकुचित करके द्रोण ने कहा, ‘‘तुम तो भली-भाँति जानते हो, तुमसे बढ़कर मेरे लिए इस संसार में कुछ नहीं है। तुम्हारे मन में कभी कोई समस्या उत्पन्न न हो, उसके लिए अपनी सारी विद्या मैंने तुम्हें दी है।’’
‘‘क्षमा करें, तात ! समस्या यही है।’’ अश्वत्थामा बीच में ही बोल उठा।
पुत्र अधीर और उतावले स्वभाव का है, यह तो द्रोण जानते ही थे, किंतु उसकी आज की अधीरता उन्हें कुछ अस्वाभाविक लगी।
‘‘फिर तो पुत्र, निस्संकोच कह ही डालो।’’
‘‘पिताजी !’’ अश्वत्थामा ने कहा, ‘‘पूरे आर्यावर्त में आप आज सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं और आप कहते हैं-आपने अपनी समस्त विद्या मुझे दी है।’’
‘हाँ, वत्स, यह सत्य है। नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे अमोघ अस्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा भी मैंने तुम्हें दी है।’
‘‘किंतु ब्रह्मशिरि विद्या के पूर्ण ज्ञान से तो मैं अनभित्र ही हूं,’’ अश्वत्थामा ने अधीरता से कहा, ‘‘और आपका परम शिष्य अर्जुन यह विद्या पूरी तरह जानता है। आपके गुरुबंधु कर्ण भी जामदग्नेय परशुराम से यह विद्या सीख आए हैं। जब तक पूर्ण ब्रह्मशिर विद्या मुझे प्राप्त न हो तब तक आर्यावर्त में मैं अजेय नहीं हो सकता। अर्जुन और कर्ण के अतिरिक्त आर्यावर्त में एक और भी वीर है, जिसके हाथ में दर्भ का तिनका भी ब्रह्मास्त्र या नारायणास्त्र से अधिक जाज्वल्यमान् बन जाती है। उस समर्थ पुरुष की विद्या....’’
‘‘तुम...तुम...कृष्ण की बात कर रहे हो, पुत्र ?’’ द्रोण बीच में ही बोल उठे।
‘‘जी हाँ, पिताजी ! कृष्ण की ओर से जब-जब देखता हूँ, हर बार मुझे लगता है, उन्होंने जो विद्या अर्जित की है, उससे मैं अभी तक कितने योजन दूर हूँ।’’
आचार्य द्रोण ने पुत्र पर किंचित् चिंता भरी दृष्टि डाली। अर्जुन और कर्ण को वह अपने समकक्ष समझकर अपना उल्लेख कर रहा था। यह कुछ सीमा तक क्षम्य था, पर उससे भी आगे बढ़कर स्वयं कृष्ण को ही अपने समकक्ष समझने लगे, यह बात उन्हें उद्वेग-प्रेरक लगी।
‘‘अश्वत्थामा !’’ द्रोण ने गंभीर स्वरं में कहा, ‘‘कृष्ण ने कोई विद्या अर्जित नहीं की, पुत्र ! वे तो स्वयं ही समस्त विद्याओं की गंगोत्तरी हैं। अर्जुन और कर्ण की श्रेणी में तो उनका नामोल्लेख भी नहीं किया जा सकता।’’ ‘‘आप जो कह रहे हैं उस सत्य को स्वीकार करते हुए भी अर्जुन और कर्ण के समकक्ष भी मैं-आर्यावर्त के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर द्रोण का पुत्र-अभी तक नहीं बन सका यह सत्य मेरे हृदय में शूल की भाँति चुभता है।’’
द्रोण थोड़े विचार में पड़ गए। पुत्र अश्वत्थामा को शिक्षा देने में उन्होंने कोई त्रुटि नहीं की थी। फिर भी पुत्र के मन में जो शूल-वेदना हो रही थी वह शूल..।
‘‘वत्स !’’ थोड़ी देर बाद द्रोण बोले, ‘‘धनुर्धारी या अन्य शस्त्रधारी को श्रेष्ठत्व प्रदान करनेवाला तत्त्व उसका शस्त्र नहीं होता। शस्त्र तो उपकरण मात्र है।
श्रेष्ठता तो उसे मन में रहनेवाले अभय के कारण प्राप्त होती है।’’
‘‘मैं समझा नहीं, पिताजी।’’
‘‘तुम्हारे मन की गहराई में अर्जुन और कर्ण की श्रेष्ठता के प्रति ईर्ष्या-भाव है। तुम संभवतः स्वयं को उनसे हीन समझते हो। यह हीनता-भाव ही तुम्हारा भय है, पुत्र ! भयभीत व्यक्ति के हाथ में श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ शस्त्र भी निरर्थक है।’’ द्रोण बोले, ‘‘सबसे पहले तुम इस भय का त्याग करो, पुत्र। अभय से बढ़कर दूसरा कोई अमोघ अस्त्र नहीं।’’
‘‘आप यह क्या कह रहे हैं, पिताजी ?’’ अश्वत्थामा ने चौंककर कहा, ‘‘मैं क्या भयभीत हूँ ?’’
‘‘मन में समाया भय ही किसी व्यक्ति को दूसरों के साथ अपनी तुलना करने की प्रेरणा देता है। एक बार इस विषचक्र से तुम स्वयं को मुक्त कर लो तो ब्रह्मशिर भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा।
‘‘क्षमा करें, पिताजी !’’ अश्वत्थामा बोल उठे, ‘‘आप जो कह रहे हैं, यदि वह सत्य है तो आपने जो विद्या अर्जित की है, क्या वह भय-प्रेरित है ? सुना है, आपने महामुनि भरद्वाज, महर्षि अग्निवेश और स्वयं जामदग्नेय परशुराम से शस्त्रास्त्र सीखे हैं। तो क्या वह भी भय-प्रेरित था ? असंभव...तात ! यह असंभव है।’’
द्रोणाचार्य के होंठों पर एक समस्या-प्रेरक स्मित प्रकट हुई। उनकी आँखें असीम आकाश में गहरे उतर गईं। थोड़ी देर बाद वे धीरे से बोले, ‘‘वत्स ! तुमने सही प्रश्न पूछा। आत्मबोध का आरंभ संभवतः ऐसे ही प्रश्नों से होता है। मेरे विद्योपार्जन कृत्य आरंभ में ब्राह्मण-धर्म का एक सहज कृत्य था, किंतु-किंतु उसके बाद...’’ द्रोण थोड़ा रुके।
‘‘उसके बाद क्या हुआ, तात ?’’
जिस दिन द्रोण प्रथम बार जामदग्नेय परशुराम के पास गए थे वह दिन उनकी आँखों के सामने आ खड़ा हुआ। अकिंचन ब्राह्मण द्रोण का परिवार उस समय घोर दरिद्रता में अपना जीवन-निर्वाह कर रहा था। दारिद्र्य ने उनके घर-संसार को इस तरह ग्रस लिया था कि अपने शिशु-पुत्र अश्वत्थामा की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरी कर पाना भी द्रोण के लिए संभव नहीं था। उसी समय उन्हें ज्ञात हुआ कि परशुराम अपनी सारी द्रव्य-संपत्ति ब्राह्मणों को दान करके पुनः एक बार तपस्या करने के लिए हिमालय जा रहे हैं। यह ज्ञात होते ही द्रोण ने सोचा, यदि परशुराम स्वयं दान-स्वरूप कुछ द्रव्य प्रदान कर रहे हों। तो उसे स्वीकार करके इस दारिद्र्य से छुटकारा पाने में क्या बुराई है ? द्रव्य-प्राप्ति की इस लालसा से प्रेरित होकर ही तो उस दिन द्रोण परशुराम के पास गए थे।
परशुराम ने ब्राह्मण द्रोण का सत्कार किया और उसके बाद कहा, ‘‘ब्राह्मण ! आप ऐसे क्षण में आए हैं जब मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर चुका हूँ। अब मेरे पास मात्र एक सम्पत्ति शेष है।’
‘तो फिर वही संपत्ति मुझे दे दीजिए, भार्गव !’’ द्रोण ने लालसा भरे स्वर में कहा।
‘यह संपत्ति तो सिंहनी का दूध है, ब्राह्मण ! इसको तो स्वर्ण पात्र में ही स्वीकार किया जा सकता है।’ परशुराम ने कहा।
‘आप विश्वास रखिए, जामदग्नेय। मैं महर्षि भरद्वाज का पुत्र हूँ। आपकी संपत्ति सुरक्षित रख सकूँ, इतना स्वर्ण मेरे पास है कि नहीं, इसकी परीक्षा हो जाने दीजिए, गुरुवर।’
‘यह संपत्ति कोई स्थूल संपत्ति नहीं है, वत्स। यह संपत्ति है-मेरी धनुर्विद्या शास्त्रों का मेरा ज्ञान।’
‘तो फिर यह ज्ञान मुझे दे दीजिए। मैं यहाँ द्रव्य की आशा से आया हूँ, खाली हाथ नहीं जाना चाहता।’
उस समय द्रोण के मन में एक अन्य लालसा भी थी। परशुराम से उन्हें तत्काल द्रव्योपार्जन भले ही नहीं हो सका, उनके पास से द्रोण को जो विद्या हस्तगत होने जा रही थी, वह भी तो अमूल्य ही थी। उसका विक्रय भले न हो सके, पर वह द्रव्योपार्जन का माध्यम तो बन ही सकती थी। विद्या को द्र्व्योपार्जन का माध्यम बनाने की इस लालसा के मूल में भी तो अश्वत्थामा ही था। पुत्र अश्वत्थामा को दारिद्र्य से मुक्त करके, लाड़-प्यार से उसका पालन-पोषण हो सके, यह पुत्र-प्रेम भी द्रोण को द्रव्य-लालसा के मार्ग पर खींच रहा था।
और आज वह अश्वत्थामा ही पिता द्रोण को उन क्षणों का स्मरण दिलाकर समस्या खड़ी कर रहा था।
‘‘इसके बाद...इसके बाद..क्या हुआ तात ?’’ द्रोणाचार्य को जाग्रत् करते हुए अश्वत्थामा ने एक बार फिर पूछा।
‘‘उसके बाद...उसके बाद जो हुआ उसके निर्णय का कार्य हम महाकाल को सौंप दें, यही इष्ट है, पुत्र !’’ बात को पूर्ण विराम दे रहे हों, इस तरह द्रोण ने कहा, ‘‘किंतु शस्त्र विद्या का एक परम सत्य कभी नहीं भूलना, वत्स !’’
‘‘कौन सा परम सत्य, पिताजी ?’’ अश्वत्थामा ने पूछा।
‘‘निस्वार्थ भाव से आततार्या या शस्त्राघात करना शस्त्रधारी वीर के लिए धर्म है, अन्यथा शस्त्र प्रहार के लिए नहीं, रक्षा के लिए ही होता है।’’
‘‘पिताजी, आप एक कठिन समस्या का निर्माण कर रहे हैं।’’
‘‘इस समस्या की जड़े देखना कहीं किसी लालसा से न जुड़ी हों।’’ द्रोण थोड़ा हँस पड़े। उन्हें स्वयं अपना अतीत याद आ रहा था।
‘‘आप जिसे लालसा कह रहे हैं, संभव है, वह महत्त्वाकांक्षा हो।’’ अश्वत्थामा ने कहा, ‘‘और महत्त्वकांक्षा कोई हीनता नहीं।’’
‘‘आकांक्षा ईश्वर के कार्यों के प्रति अविश्वास के अतिरिक्त और कुछ नहीं, वत्स ! ईश्वर ने जिस व्यवस्था का निर्माण किया है उसके प्रति असंतोष ही आकांक्षा का असली रूप है। एक बार हम ईश्वर की व्यवस्था को स्वीकार कर लें तो हमारे भीतर कोई आकांक्षा रह ही नहीं जाती और आकांक्षा का अवसान हो जाने पर लालसा का उद्भव ही कैसे होगा ?’’
‘‘यह दर्शन मेरे लिए नितांत नया है, तात ! इसका अंगीकार मुझसे संभवतः समय ही करवा सकेगा।’’
‘‘हाँ, पुत्र, समय ही मुझसे यह काम करवा सका है।’’
अश्वत्थामा मौन हो गया।
थोड़ी दूर, आवास के मुख्य प्रवेश-द्वार के पास, खड़े प्रहरियों में से एक उनकी तरफ आ रहा था। द्रोण ने उस ओर देखा। प्रहरी निकट आया। द्रोण के सम्मुख खड़े रहकर उसने वंदन किया और फिर बोला, ‘‘आचार्य ! महर्षि उपजाय पधारे हैं।’’
‘‘उपयाज ! यहाँ ? इस समय ?’’ द्रोण को आचार्य हुआ। अभी कुछ ही देर पहले तो पुत्र अश्वत्थामा के प्रश्न के संदर्भ में उन्होंने ही जामदग्नेय परशुराम का स्मरण किया था। अभी तक वह स्मृति ताजा ही है, इस बीच अतीत की यह दूसरी स्मृति।
‘‘जाओ,’’ द्रोण ने त्वरित निर्णय लिया, ‘‘महर्षि उपयाज को ससम्मान यहाँ ले आओ और..और पुत्र अश्वत्थामा !’’ द्रोण ने पुत्र को आदेश दिया, ‘‘स्वाध्याय-कक्ष में से शिष्यों को तुम्हीं पटांगण में ले जाओ। मैं महर्षि के स्वागत में व्यस्त रहूँगा। अपनी माता को संदेश भेजो कि महर्षि के स्वागत के लिए यथोचित सामग्री के साथ यहाँ उपस्थित हों।’’
प्रहरी ने पीठ फेरी।
अश्वत्थामा ने भी कदम बढ़ाए।
द्रोण खड़े हुए।
नगर की पूर्व सीमा से प्रवेश करते ही कुछ कदम चलने के बाद एक सुंदर पगडंडी मुख्य मार्ग से फूट निकलती थी। इस पगडंडी पर एक ऐसा आवास दिखाई देता था, जिसे महालय कहें तो तपोवन लगे और तपो वन कहें तो उसके महालय होने की साक्षी देते तत्त्व उड़कर आँखों में गड़ने लगें। प्रांगण में ही लगे ध्वज में विचित्र-वेद ग्रंथों और कमंडलु के चित्र इस आवास में रहनेवालों के ज्ञान और त्याग के प्रतीक लग रहे थे। विशाल प्रांगण के ठीक मध्य में प्रज्वलित यज्ञवेदी के समीप ही एक विशाल चौकी पर दृष्टि पड़ते ही जिसके प्रभाव में आ जाए, ऐसा एक धनुष रखा हुआ था। यज्ञवेदी से निकलती धूम-रेखाओं के साथ ही इस धनुष का पूजन भी अभी-अभी होने का प्रमाण देते पुष्प उसके ऊपर फैले हुए थे।
यह आवास आचार्य द्रोण का था।
प्रातः संध्या और धनुष-पूजन से निवृत्त होकर आचार्य द्रोण अपने नित्य के आसन की ओर घूमे। यज्ञवेदी से कुछ ही दूर एक विशाल वृक्ष के नीचे काष्ट की एक ऊँची चौकी पर व्याघ्र-चर्म बिछाकर पुत्र अश्वात्थामा पिता के आसनस्थ होने की प्रतीक्षा में खड़ा था। स्वाध्याय-कक्ष में बैठकर शिष्यगण प्रतिदिन प्रातः विद्याध्ययन में प्रवृत्त होते तो उस समय द्रोण प्रातः संध्या पूर्ण करते। सूर्य किरणों के पूरी तरह फैल जाने तक स्वाध्याय-कक्ष में वेदाध्ययन चलता रहता। वेदाध्ययन के अंत में शांति-पाठ होता और उसके बाद सभी शिष्य बाहर पटांगण में आकर शस्त्राभ्यास करते। कोई गज-विद्या, कोई रथ-विद्या कोई गदा-युद्ध तो कोई खड्ग-युद्ध में निपुणता प्राप्त करने के लिए आचार्य के सम्मुख उपस्थित होता। उन सबको आचार्य द्रोण पुत्रवत् स्नेह देकर विद्याभ्यास कराते। इस शिष्य समूह में कई राजपुत्र थे तो कई ऐसे ब्राह्मण-पुत्र भी थे, जिन्होंने स्वेच्छया क्षात्र धर्म स्वीकार कर लिया था। कुरुवंश के आचार्य पद पर स्थापित होने के बाद द्रोणाचार्य की प्रतिष्ठा आर्यावर्त में बहुत बढ़ गई थी। तिस पर उनके पट्ट शिष्य अर्जुन के नेतृत्व में कौरवों और पांडवों ने मिलकर पांचाल-नरेश द्रुपद का जिस तरह पराभव किया था, उसकी कथा तो उत्तरापथ में एक किंवदंती ही बन गई थी।
धीमे, पर दृढ़ से द्रोण अपने व्याघ्र-चर्म बिछे आसन की ओर चले तो आसन के समीप तनकर खड़े अश्वत्थामा ने सहज ही अपना मस्तक किंचित् झुका दिया। द्रोण आसनस्थ हुए, वात्सल्यपूरित दृष्टि से पुत्र की ओर देखा। होंठ फड़काकर कोई मंत्रोच्चार किया और आँखें मूँद लीं।
‘‘तात !’’ अश्वत्थामा का स्वर नीरव शांति के बीच प्रकट हुआ।
द्रोण ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि से प्रश्न परिलक्षित था। द्रोण के आसनस्थ होने के पश्चात् अश्वत्थाना प्रतिदिन स्वाध्याय-कक्ष में लौट जाते थे। आज उसका इस तरह खड़ा रह जाना असामान्य था। आचार्य ने पुत्र पर दृष्टि स्थिर की। अश्वत्थामा की ताम्रवर्णी काया से मानो शक्ति और उत्साह का सागर उमड़ रहा था।
‘‘तुम कुछ बोले, वत्स ?’’ द्रोण ने धीरे से पूछा।
‘‘पिताजी !’’ अश्वत्थामा बोले, ‘‘एक शंका का समाधान चाहता हूँ।’’
‘‘शंका ?’’ द्रोण उठकर हँस पड़े।
‘‘जी हाँ ! मेरे मन में एक प्रश्न सदैव अनुत्तरित रहा है।’’
‘‘प्रश्न का उद्गम-स्थल यदि गंगोत्तरी जैसा पवित्र हो तो प्रश्न तो सदैव उपनिषदों की पूर्व भूमिका रहे हैं, पुत्र !’’ द्रोणाचार्य के होंठों पर किंचित् हास्य खेल गया।
‘‘मेरा प्रश्न इस उच्च स्तर का है कि नहीं, मैं यह नहीं जानता, पिताजी ! आपका आदेश हो तो मन में घुमड़ रही अपनी समस्या मैं आपके समक्ष प्रकट करूँ।’’
‘‘वत्स !’’ थोड़ा रुककर अपने नेत्र संकुचित करके द्रोण ने कहा, ‘‘तुम तो भली-भाँति जानते हो, तुमसे बढ़कर मेरे लिए इस संसार में कुछ नहीं है। तुम्हारे मन में कभी कोई समस्या उत्पन्न न हो, उसके लिए अपनी सारी विद्या मैंने तुम्हें दी है।’’
‘‘क्षमा करें, तात ! समस्या यही है।’’ अश्वत्थामा बीच में ही बोल उठा।
पुत्र अधीर और उतावले स्वभाव का है, यह तो द्रोण जानते ही थे, किंतु उसकी आज की अधीरता उन्हें कुछ अस्वाभाविक लगी।
‘‘फिर तो पुत्र, निस्संकोच कह ही डालो।’’
‘‘पिताजी !’’ अश्वत्थामा ने कहा, ‘‘पूरे आर्यावर्त में आप आज सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं और आप कहते हैं-आपने अपनी समस्त विद्या मुझे दी है।’’
‘हाँ, वत्स, यह सत्य है। नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे अमोघ अस्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा भी मैंने तुम्हें दी है।’
‘‘किंतु ब्रह्मशिरि विद्या के पूर्ण ज्ञान से तो मैं अनभित्र ही हूं,’’ अश्वत्थामा ने अधीरता से कहा, ‘‘और आपका परम शिष्य अर्जुन यह विद्या पूरी तरह जानता है। आपके गुरुबंधु कर्ण भी जामदग्नेय परशुराम से यह विद्या सीख आए हैं। जब तक पूर्ण ब्रह्मशिर विद्या मुझे प्राप्त न हो तब तक आर्यावर्त में मैं अजेय नहीं हो सकता। अर्जुन और कर्ण के अतिरिक्त आर्यावर्त में एक और भी वीर है, जिसके हाथ में दर्भ का तिनका भी ब्रह्मास्त्र या नारायणास्त्र से अधिक जाज्वल्यमान् बन जाती है। उस समर्थ पुरुष की विद्या....’’
‘‘तुम...तुम...कृष्ण की बात कर रहे हो, पुत्र ?’’ द्रोण बीच में ही बोल उठे।
‘‘जी हाँ, पिताजी ! कृष्ण की ओर से जब-जब देखता हूँ, हर बार मुझे लगता है, उन्होंने जो विद्या अर्जित की है, उससे मैं अभी तक कितने योजन दूर हूँ।’’
आचार्य द्रोण ने पुत्र पर किंचित् चिंता भरी दृष्टि डाली। अर्जुन और कर्ण को वह अपने समकक्ष समझकर अपना उल्लेख कर रहा था। यह कुछ सीमा तक क्षम्य था, पर उससे भी आगे बढ़कर स्वयं कृष्ण को ही अपने समकक्ष समझने लगे, यह बात उन्हें उद्वेग-प्रेरक लगी।
‘‘अश्वत्थामा !’’ द्रोण ने गंभीर स्वरं में कहा, ‘‘कृष्ण ने कोई विद्या अर्जित नहीं की, पुत्र ! वे तो स्वयं ही समस्त विद्याओं की गंगोत्तरी हैं। अर्जुन और कर्ण की श्रेणी में तो उनका नामोल्लेख भी नहीं किया जा सकता।’’ ‘‘आप जो कह रहे हैं उस सत्य को स्वीकार करते हुए भी अर्जुन और कर्ण के समकक्ष भी मैं-आर्यावर्त के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर द्रोण का पुत्र-अभी तक नहीं बन सका यह सत्य मेरे हृदय में शूल की भाँति चुभता है।’’
द्रोण थोड़े विचार में पड़ गए। पुत्र अश्वत्थामा को शिक्षा देने में उन्होंने कोई त्रुटि नहीं की थी। फिर भी पुत्र के मन में जो शूल-वेदना हो रही थी वह शूल..।
‘‘वत्स !’’ थोड़ी देर बाद द्रोण बोले, ‘‘धनुर्धारी या अन्य शस्त्रधारी को श्रेष्ठत्व प्रदान करनेवाला तत्त्व उसका शस्त्र नहीं होता। शस्त्र तो उपकरण मात्र है।
श्रेष्ठता तो उसे मन में रहनेवाले अभय के कारण प्राप्त होती है।’’
‘‘मैं समझा नहीं, पिताजी।’’
‘‘तुम्हारे मन की गहराई में अर्जुन और कर्ण की श्रेष्ठता के प्रति ईर्ष्या-भाव है। तुम संभवतः स्वयं को उनसे हीन समझते हो। यह हीनता-भाव ही तुम्हारा भय है, पुत्र ! भयभीत व्यक्ति के हाथ में श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ शस्त्र भी निरर्थक है।’’ द्रोण बोले, ‘‘सबसे पहले तुम इस भय का त्याग करो, पुत्र। अभय से बढ़कर दूसरा कोई अमोघ अस्त्र नहीं।’’
‘‘आप यह क्या कह रहे हैं, पिताजी ?’’ अश्वत्थामा ने चौंककर कहा, ‘‘मैं क्या भयभीत हूँ ?’’
‘‘मन में समाया भय ही किसी व्यक्ति को दूसरों के साथ अपनी तुलना करने की प्रेरणा देता है। एक बार इस विषचक्र से तुम स्वयं को मुक्त कर लो तो ब्रह्मशिर भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा।
‘‘क्षमा करें, पिताजी !’’ अश्वत्थामा बोल उठे, ‘‘आप जो कह रहे हैं, यदि वह सत्य है तो आपने जो विद्या अर्जित की है, क्या वह भय-प्रेरित है ? सुना है, आपने महामुनि भरद्वाज, महर्षि अग्निवेश और स्वयं जामदग्नेय परशुराम से शस्त्रास्त्र सीखे हैं। तो क्या वह भी भय-प्रेरित था ? असंभव...तात ! यह असंभव है।’’
द्रोणाचार्य के होंठों पर एक समस्या-प्रेरक स्मित प्रकट हुई। उनकी आँखें असीम आकाश में गहरे उतर गईं। थोड़ी देर बाद वे धीरे से बोले, ‘‘वत्स ! तुमने सही प्रश्न पूछा। आत्मबोध का आरंभ संभवतः ऐसे ही प्रश्नों से होता है। मेरे विद्योपार्जन कृत्य आरंभ में ब्राह्मण-धर्म का एक सहज कृत्य था, किंतु-किंतु उसके बाद...’’ द्रोण थोड़ा रुके।
‘‘उसके बाद क्या हुआ, तात ?’’
जिस दिन द्रोण प्रथम बार जामदग्नेय परशुराम के पास गए थे वह दिन उनकी आँखों के सामने आ खड़ा हुआ। अकिंचन ब्राह्मण द्रोण का परिवार उस समय घोर दरिद्रता में अपना जीवन-निर्वाह कर रहा था। दारिद्र्य ने उनके घर-संसार को इस तरह ग्रस लिया था कि अपने शिशु-पुत्र अश्वत्थामा की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरी कर पाना भी द्रोण के लिए संभव नहीं था। उसी समय उन्हें ज्ञात हुआ कि परशुराम अपनी सारी द्रव्य-संपत्ति ब्राह्मणों को दान करके पुनः एक बार तपस्या करने के लिए हिमालय जा रहे हैं। यह ज्ञात होते ही द्रोण ने सोचा, यदि परशुराम स्वयं दान-स्वरूप कुछ द्रव्य प्रदान कर रहे हों। तो उसे स्वीकार करके इस दारिद्र्य से छुटकारा पाने में क्या बुराई है ? द्रव्य-प्राप्ति की इस लालसा से प्रेरित होकर ही तो उस दिन द्रोण परशुराम के पास गए थे।
परशुराम ने ब्राह्मण द्रोण का सत्कार किया और उसके बाद कहा, ‘‘ब्राह्मण ! आप ऐसे क्षण में आए हैं जब मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर चुका हूँ। अब मेरे पास मात्र एक सम्पत्ति शेष है।’
‘तो फिर वही संपत्ति मुझे दे दीजिए, भार्गव !’’ द्रोण ने लालसा भरे स्वर में कहा।
‘यह संपत्ति तो सिंहनी का दूध है, ब्राह्मण ! इसको तो स्वर्ण पात्र में ही स्वीकार किया जा सकता है।’ परशुराम ने कहा।
‘आप विश्वास रखिए, जामदग्नेय। मैं महर्षि भरद्वाज का पुत्र हूँ। आपकी संपत्ति सुरक्षित रख सकूँ, इतना स्वर्ण मेरे पास है कि नहीं, इसकी परीक्षा हो जाने दीजिए, गुरुवर।’
‘यह संपत्ति कोई स्थूल संपत्ति नहीं है, वत्स। यह संपत्ति है-मेरी धनुर्विद्या शास्त्रों का मेरा ज्ञान।’
‘तो फिर यह ज्ञान मुझे दे दीजिए। मैं यहाँ द्रव्य की आशा से आया हूँ, खाली हाथ नहीं जाना चाहता।’
उस समय द्रोण के मन में एक अन्य लालसा भी थी। परशुराम से उन्हें तत्काल द्रव्योपार्जन भले ही नहीं हो सका, उनके पास से द्रोण को जो विद्या हस्तगत होने जा रही थी, वह भी तो अमूल्य ही थी। उसका विक्रय भले न हो सके, पर वह द्रव्योपार्जन का माध्यम तो बन ही सकती थी। विद्या को द्र्व्योपार्जन का माध्यम बनाने की इस लालसा के मूल में भी तो अश्वत्थामा ही था। पुत्र अश्वत्थामा को दारिद्र्य से मुक्त करके, लाड़-प्यार से उसका पालन-पोषण हो सके, यह पुत्र-प्रेम भी द्रोण को द्रव्य-लालसा के मार्ग पर खींच रहा था।
और आज वह अश्वत्थामा ही पिता द्रोण को उन क्षणों का स्मरण दिलाकर समस्या खड़ी कर रहा था।
‘‘इसके बाद...इसके बाद..क्या हुआ तात ?’’ द्रोणाचार्य को जाग्रत् करते हुए अश्वत्थामा ने एक बार फिर पूछा।
‘‘उसके बाद...उसके बाद जो हुआ उसके निर्णय का कार्य हम महाकाल को सौंप दें, यही इष्ट है, पुत्र !’’ बात को पूर्ण विराम दे रहे हों, इस तरह द्रोण ने कहा, ‘‘किंतु शस्त्र विद्या का एक परम सत्य कभी नहीं भूलना, वत्स !’’
‘‘कौन सा परम सत्य, पिताजी ?’’ अश्वत्थामा ने पूछा।
‘‘निस्वार्थ भाव से आततार्या या शस्त्राघात करना शस्त्रधारी वीर के लिए धर्म है, अन्यथा शस्त्र प्रहार के लिए नहीं, रक्षा के लिए ही होता है।’’
‘‘पिताजी, आप एक कठिन समस्या का निर्माण कर रहे हैं।’’
‘‘इस समस्या की जड़े देखना कहीं किसी लालसा से न जुड़ी हों।’’ द्रोण थोड़ा हँस पड़े। उन्हें स्वयं अपना अतीत याद आ रहा था।
‘‘आप जिसे लालसा कह रहे हैं, संभव है, वह महत्त्वाकांक्षा हो।’’ अश्वत्थामा ने कहा, ‘‘और महत्त्वकांक्षा कोई हीनता नहीं।’’
‘‘आकांक्षा ईश्वर के कार्यों के प्रति अविश्वास के अतिरिक्त और कुछ नहीं, वत्स ! ईश्वर ने जिस व्यवस्था का निर्माण किया है उसके प्रति असंतोष ही आकांक्षा का असली रूप है। एक बार हम ईश्वर की व्यवस्था को स्वीकार कर लें तो हमारे भीतर कोई आकांक्षा रह ही नहीं जाती और आकांक्षा का अवसान हो जाने पर लालसा का उद्भव ही कैसे होगा ?’’
‘‘यह दर्शन मेरे लिए नितांत नया है, तात ! इसका अंगीकार मुझसे संभवतः समय ही करवा सकेगा।’’
‘‘हाँ, पुत्र, समय ही मुझसे यह काम करवा सका है।’’
अश्वत्थामा मौन हो गया।
थोड़ी दूर, आवास के मुख्य प्रवेश-द्वार के पास, खड़े प्रहरियों में से एक उनकी तरफ आ रहा था। द्रोण ने उस ओर देखा। प्रहरी निकट आया। द्रोण के सम्मुख खड़े रहकर उसने वंदन किया और फिर बोला, ‘‘आचार्य ! महर्षि उपजाय पधारे हैं।’’
‘‘उपयाज ! यहाँ ? इस समय ?’’ द्रोण को आचार्य हुआ। अभी कुछ ही देर पहले तो पुत्र अश्वत्थामा के प्रश्न के संदर्भ में उन्होंने ही जामदग्नेय परशुराम का स्मरण किया था। अभी तक वह स्मृति ताजा ही है, इस बीच अतीत की यह दूसरी स्मृति।
‘‘जाओ,’’ द्रोण ने त्वरित निर्णय लिया, ‘‘महर्षि उपयाज को ससम्मान यहाँ ले आओ और..और पुत्र अश्वत्थामा !’’ द्रोण ने पुत्र को आदेश दिया, ‘‘स्वाध्याय-कक्ष में से शिष्यों को तुम्हीं पटांगण में ले जाओ। मैं महर्षि के स्वागत में व्यस्त रहूँगा। अपनी माता को संदेश भेजो कि महर्षि के स्वागत के लिए यथोचित सामग्री के साथ यहाँ उपस्थित हों।’’
प्रहरी ने पीठ फेरी।
अश्वत्थामा ने भी कदम बढ़ाए।
द्रोण खड़े हुए।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book