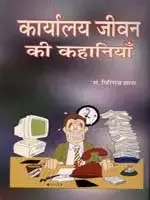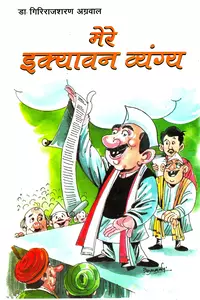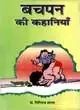|
हास्य-व्यंग्य >> कार्यालय जीवन की कहानियाँ कार्यालय जीवन की कहानियाँगिरिराजशरण अग्रवाल
|
68 पाठक हैं |
||||||
कार्यालय जीवन की कहानियाँ
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
कार्यालयी संस्कृति के विशद इंद्रजाल से मोहित समाज की विवशता प्रायः
लेखकों और कहानीकारों की लेखनी का विषय रही है, और कथाकारों ने व्यापक फलक
पर इस संस्कृति के सच्चे या यथार्थ चित्र उकेरे हैं, जिनमें नैतिक मूल्यों
के ह्रास का रूपांकन करते समय उन्होने कार्यालयी वास्तविकता के रंगों को
अधिक से अधिक गहरा करने का प्रयास किया है। इस संग्रह में ऐसे ही कुछ
विशिष्ट कथाचित्र समाविष्ट है।
कार्यालयों का इंद्रजाल
विद्युत विभाग को कार्यालय तक पहुंचने से पहले ही मुझे कई शाश्वत नारे
सुनाई दिए-
‘‘हमारी मांगें पूरी करो’’
‘‘जितना वेतन, उतना काम’’
‘‘जो हमसे टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा’’
गेट तक पहुंचते-पहुंचते मुझे लगा जैसे कि मैं किसी बड़ी भीड़ का हिस्सा बन गया हूं। इतने आदमी तो मैंने इस कार्यालय में आज तक नहीं देखे थे-क्या इनका अवतार आज ही हुआ है अथवा ये सब अपनी कुर्सियों के अदृश्य भागों से आज अचानक प्रकट हो गए हैं ? कल भी तो आया था मैं। तब तो कुर्सियां थीं, फाइलें थीं, टाइप मशीन और अलमारियां थीं किंतु उनके साथ केलिक्रीड़ा करने वाले अधिकांश मनमोहन गायब थे। तब किसी ने कहा था कि कैन्टीन-कुंज में जाइए। सभी गोप-ग्वाले वहीं मिलेंगे। मैंने देखा था कि सभी अपनी-अपनी गायों को दुहने में लगे हैं।
दोहन को तत्पर कृष्ण-क्लर्क की मायावी आंखों ने मुझे इंद्रजाल में बांध लिया और मैं बंध गया।
आज उसी मनमोहन को खोजने पहुंचा था मैं। दुग्ध-धवल चांदनी पर श्वेत-श्याम वस्त्रालंकृत मेरे घनश्याम का वक्षस्थल पुष्पमालाओं से परिपूर्ण था। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा और फिर दोनों ने स्वयं को देखकर ऐसे देखा-मानो किसी ने भी किसी को न देखा हो। मैंने सोचा-क्या होगा इस देश का ? नहीं, नहीं, क्या होगा मेरा ? अंतर्द्वन्द्व के जंगल में भटक गया था मैं। कैन्टीन की एक खाली बैंच पर बैठकर मैंने सोचा-सामाजिक व्यवस्था और वर्गीकरण का इतिहास रोचक भी है और शिक्षाप्रद भी। दूर अतीत के मानव-समाज में आदमी वर्गों से जीविका अर्जित करता था और मिल-बांटकर उसका उपभोग करता था। यह हजारों वर्ष पहले की बात है, तब लोग विभिन्न समूहों में एक साथ रहते, बसते और जीवन-निर्वाह करते थे। मानव-सभ्यता के विकास की यह स्थिति सैकड़ों वर्ष तक बनी रही। धीरे-धीरे इतिहास दो अध्यायों में बंट गया-एक का रिश्ता शारीरिक श्रम करने वाले समूह से था तो दूसरे का उनसे, जिन्होंने उत्पादन के अधिकार साधनों पर अपना अधिकार कर लिया था। यथार्थवादी विचारक इस बात को स्वीकार करें या न करें किंतु वास्तविकता यही है कि समाज का वह वर्ग, जिसने शारीरिक, मानसिक और भौतिक शक्ति अर्जित कर ली थी, उन समूहों पर अपने अधिकार को आरोपित करता गया, जो इनसे वंचित थे।
एक दर्शनिक ने इस स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा था कि अस्त्र निर्मित करने के तुरंत बाद अस्त्र-निर्माता के हाथ दूसरों की अपेक्षा इतने लंबे हो गए कि वह सीमित हाथ वाले व्यक्तियों की गर्दन तक सरलता से पहुंच सकते थे। दार्शनिक का तात्पर्य यही है कि समाज का वह वर्ग, जिसने अस्त्र-शस्त्र और उत्पादन के अन्य साधनों को शारीरिक शक्ति या विवेक से एकत्र किया, दूसरे दुर्बल लोगों को अपना दास बनाता गया। लेकिन कारण क्या था ?
मनोविज्ञान का अध्ययन बताता है कि आदमी यह बात भली प्रकार समझ गया था कि वह अपने जैसे दूसरे व्यक्तियों की मेहनत से ही विलासिता के साधन जुटा सकता है। तब उसने भौतिक-मानसिक शक्ति के बल, अन्य लोगों की मेहनत से, अपने लिए सुविधाएँ जुटाईं और स्वयं किसी समूह का अधिकारी बनकर उन पर शासन करने लगा। इतिहास यह भी बताता है कि अपने श्रम से सरदार के लिए सुख-सुविधाओं को जुटाने वाले लोग बार-बार विद्रोह करते रहे हैं और दासता के इस जुए को उतार फेंककर स्वतंत्र हो जाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। श्रमिकों के सुसंगठित समूह विद्रोह करके या तो अपने स्वामी और सरदार के बंधन से मुक्त हो गए अथवा उनके सर कलम कर दिए गए। इस अराजकता को नियंत्रित करने के लिए और समूहों को अनुशासित रखने के लिए तब एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव हुई, जिसके द्वारा शासित जनता को बांधकर रखा जा सके। यही वह काल है जब कार्यालयी सभ्यता का जन्म हुआ। इस प्रकार श्रमिक और स्वामी के मध्य एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो गई, जो एक-दूसरे को अपने व्यवहार और कार्यपद्धति के प्रति उत्तरदायी बनाती थी।
इतिहास के मध्यकाल तक पहुंचते-पहुंचते श्रमिक और स्वामी के बीच पुल का काम देने वाली यह व्यवस्था मानव-समाज की आवश्यकता बन गई। अब एक ऐसा वर्ग अस्तित्व में आया जो स्वयं साधनहीन था किंतु उसकी नियुक्ति इसलिए की जाती थी ताकि जनसाधारण सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध किसी प्रकार का विद्रोह न कर सके। यही कार्यप्रणाली हमारे युग में कार्यालयी-सभ्यता का रूप धारण कर एक विशेष वर्ग की मानसिकता की द्योतक बन गई है।
मुझे याद आया-जब केंद्रीय वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं देने के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर रहा था तो भारत के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने बहुत ही दिलचस्प टिप्पणी की थी। उसने कहा था कि भारत की कुल जनसंख्या का दस प्रतिशत भाग, जिसे वेतनभोगी कर्मचारी कहा जाता है, आज नब्बे प्रतिशत जनता पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहा है। यह बात आश्चर्यजनक जरूर है कि इतिहास के इस यात्रा-क्रम में, उत्पादनकर्ता और उपभोक्ताओं से भी अधिक महत्त्व उस वर्ग ने प्राप्त कर लिया है, जिसके पास पहले न तो शक्ति थी और न साधन। वह केवल एक ऐसा मध्यस्थ था जिसे व्यवस्थापकों और व्यस्था के अंतर्गत जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सृजित किया गया था।
इक्कीसवीं सदी की दहलीज पर खड़े हम प्रतिदिन यह तमाशा देखते रहे हैं कि हमारे सामाजिक जीवन की सारी बागडोर आज इसी कर्मचारी-वर्ग के हाथ में हैं; और इसका अंकुश ऊपर से नीचे तक इतना मजबूत है कि शासक से लेकर शासित तक, कोई उससे मुक्त नहीं है।
आज, जबकि कार्यालय आधुनिक जीवन के महत्त्वपूर्ण अंग बन चुके हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आधुनिक सभ्यता और संस्कृति पर कार्यालयी-कल्चर का गहरा रंग चढ़ता जा रहा है। दफ्तर के ‘बाबू संप्रदाय’ की मानसिकता को समाज द्वारा जाने-अनजाने मान्यता मिलती गई है। इसका एक दुःखद पहलू यह भी है कि आधुनिक बाबू समाज की विशेष सभ्यता के साथ जो विचित्र ‘गुण’ आए हैं, वे भी कुछ समस्त समाज ने बिना किसी आपत्ति के मौन भाव से स्वीकार कर लिए हैं।
शायद मुझे बहुत देर हो गई थी। लड़का दो बार पानी रख गया था। इस बार उसने पूछा-‘‘बाबू जी चाय ले आऊँ ?’ अचानक के इस प्रश्न से मेरे मस्तक पर दस्तक देते हुए बड़े-बड़े सवालों का हाथ रुक गया।
भारी कदमों से मैं उठा। नारे अब भी लग रहे थे, मांगें अभी भी रखी जा रही थीं, किसी यूनियन नेता का भाषण अब भी चल रहा था।
कार्यालयी-संस्कृति के विशद् इंद्रजाल से मोहित समाज की विवशता अनेक लेखकों और कहानीकारों की लेखनी का विषय रही है और कथाकारों ने व्यापक फलक पर इस संस्कृति के सच्चे व यथार्थ चित्र उकेरे हैं जिनमें नैतिक मूल्यों के ह्रास का रूपांकन करते समय उन्होंने कार्यालयी वास्तविकता के रंगों को अधिक-से-अधिक गहरा करने का प्रयास किया है।
इस संग्रह में कुछ ऐसे ही विशिष्ट कथाचित्र संगृहीत हैं।
‘‘हमारी मांगें पूरी करो’’
‘‘जितना वेतन, उतना काम’’
‘‘जो हमसे टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा’’
गेट तक पहुंचते-पहुंचते मुझे लगा जैसे कि मैं किसी बड़ी भीड़ का हिस्सा बन गया हूं। इतने आदमी तो मैंने इस कार्यालय में आज तक नहीं देखे थे-क्या इनका अवतार आज ही हुआ है अथवा ये सब अपनी कुर्सियों के अदृश्य भागों से आज अचानक प्रकट हो गए हैं ? कल भी तो आया था मैं। तब तो कुर्सियां थीं, फाइलें थीं, टाइप मशीन और अलमारियां थीं किंतु उनके साथ केलिक्रीड़ा करने वाले अधिकांश मनमोहन गायब थे। तब किसी ने कहा था कि कैन्टीन-कुंज में जाइए। सभी गोप-ग्वाले वहीं मिलेंगे। मैंने देखा था कि सभी अपनी-अपनी गायों को दुहने में लगे हैं।
दोहन को तत्पर कृष्ण-क्लर्क की मायावी आंखों ने मुझे इंद्रजाल में बांध लिया और मैं बंध गया।
आज उसी मनमोहन को खोजने पहुंचा था मैं। दुग्ध-धवल चांदनी पर श्वेत-श्याम वस्त्रालंकृत मेरे घनश्याम का वक्षस्थल पुष्पमालाओं से परिपूर्ण था। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा और फिर दोनों ने स्वयं को देखकर ऐसे देखा-मानो किसी ने भी किसी को न देखा हो। मैंने सोचा-क्या होगा इस देश का ? नहीं, नहीं, क्या होगा मेरा ? अंतर्द्वन्द्व के जंगल में भटक गया था मैं। कैन्टीन की एक खाली बैंच पर बैठकर मैंने सोचा-सामाजिक व्यवस्था और वर्गीकरण का इतिहास रोचक भी है और शिक्षाप्रद भी। दूर अतीत के मानव-समाज में आदमी वर्गों से जीविका अर्जित करता था और मिल-बांटकर उसका उपभोग करता था। यह हजारों वर्ष पहले की बात है, तब लोग विभिन्न समूहों में एक साथ रहते, बसते और जीवन-निर्वाह करते थे। मानव-सभ्यता के विकास की यह स्थिति सैकड़ों वर्ष तक बनी रही। धीरे-धीरे इतिहास दो अध्यायों में बंट गया-एक का रिश्ता शारीरिक श्रम करने वाले समूह से था तो दूसरे का उनसे, जिन्होंने उत्पादन के अधिकार साधनों पर अपना अधिकार कर लिया था। यथार्थवादी विचारक इस बात को स्वीकार करें या न करें किंतु वास्तविकता यही है कि समाज का वह वर्ग, जिसने शारीरिक, मानसिक और भौतिक शक्ति अर्जित कर ली थी, उन समूहों पर अपने अधिकार को आरोपित करता गया, जो इनसे वंचित थे।
एक दर्शनिक ने इस स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा था कि अस्त्र निर्मित करने के तुरंत बाद अस्त्र-निर्माता के हाथ दूसरों की अपेक्षा इतने लंबे हो गए कि वह सीमित हाथ वाले व्यक्तियों की गर्दन तक सरलता से पहुंच सकते थे। दार्शनिक का तात्पर्य यही है कि समाज का वह वर्ग, जिसने अस्त्र-शस्त्र और उत्पादन के अन्य साधनों को शारीरिक शक्ति या विवेक से एकत्र किया, दूसरे दुर्बल लोगों को अपना दास बनाता गया। लेकिन कारण क्या था ?
मनोविज्ञान का अध्ययन बताता है कि आदमी यह बात भली प्रकार समझ गया था कि वह अपने जैसे दूसरे व्यक्तियों की मेहनत से ही विलासिता के साधन जुटा सकता है। तब उसने भौतिक-मानसिक शक्ति के बल, अन्य लोगों की मेहनत से, अपने लिए सुविधाएँ जुटाईं और स्वयं किसी समूह का अधिकारी बनकर उन पर शासन करने लगा। इतिहास यह भी बताता है कि अपने श्रम से सरदार के लिए सुख-सुविधाओं को जुटाने वाले लोग बार-बार विद्रोह करते रहे हैं और दासता के इस जुए को उतार फेंककर स्वतंत्र हो जाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। श्रमिकों के सुसंगठित समूह विद्रोह करके या तो अपने स्वामी और सरदार के बंधन से मुक्त हो गए अथवा उनके सर कलम कर दिए गए। इस अराजकता को नियंत्रित करने के लिए और समूहों को अनुशासित रखने के लिए तब एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव हुई, जिसके द्वारा शासित जनता को बांधकर रखा जा सके। यही वह काल है जब कार्यालयी सभ्यता का जन्म हुआ। इस प्रकार श्रमिक और स्वामी के मध्य एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो गई, जो एक-दूसरे को अपने व्यवहार और कार्यपद्धति के प्रति उत्तरदायी बनाती थी।
इतिहास के मध्यकाल तक पहुंचते-पहुंचते श्रमिक और स्वामी के बीच पुल का काम देने वाली यह व्यवस्था मानव-समाज की आवश्यकता बन गई। अब एक ऐसा वर्ग अस्तित्व में आया जो स्वयं साधनहीन था किंतु उसकी नियुक्ति इसलिए की जाती थी ताकि जनसाधारण सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध किसी प्रकार का विद्रोह न कर सके। यही कार्यप्रणाली हमारे युग में कार्यालयी-सभ्यता का रूप धारण कर एक विशेष वर्ग की मानसिकता की द्योतक बन गई है।
मुझे याद आया-जब केंद्रीय वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं देने के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर रहा था तो भारत के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने बहुत ही दिलचस्प टिप्पणी की थी। उसने कहा था कि भारत की कुल जनसंख्या का दस प्रतिशत भाग, जिसे वेतनभोगी कर्मचारी कहा जाता है, आज नब्बे प्रतिशत जनता पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहा है। यह बात आश्चर्यजनक जरूर है कि इतिहास के इस यात्रा-क्रम में, उत्पादनकर्ता और उपभोक्ताओं से भी अधिक महत्त्व उस वर्ग ने प्राप्त कर लिया है, जिसके पास पहले न तो शक्ति थी और न साधन। वह केवल एक ऐसा मध्यस्थ था जिसे व्यवस्थापकों और व्यस्था के अंतर्गत जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सृजित किया गया था।
इक्कीसवीं सदी की दहलीज पर खड़े हम प्रतिदिन यह तमाशा देखते रहे हैं कि हमारे सामाजिक जीवन की सारी बागडोर आज इसी कर्मचारी-वर्ग के हाथ में हैं; और इसका अंकुश ऊपर से नीचे तक इतना मजबूत है कि शासक से लेकर शासित तक, कोई उससे मुक्त नहीं है।
आज, जबकि कार्यालय आधुनिक जीवन के महत्त्वपूर्ण अंग बन चुके हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आधुनिक सभ्यता और संस्कृति पर कार्यालयी-कल्चर का गहरा रंग चढ़ता जा रहा है। दफ्तर के ‘बाबू संप्रदाय’ की मानसिकता को समाज द्वारा जाने-अनजाने मान्यता मिलती गई है। इसका एक दुःखद पहलू यह भी है कि आधुनिक बाबू समाज की विशेष सभ्यता के साथ जो विचित्र ‘गुण’ आए हैं, वे भी कुछ समस्त समाज ने बिना किसी आपत्ति के मौन भाव से स्वीकार कर लिए हैं।
शायद मुझे बहुत देर हो गई थी। लड़का दो बार पानी रख गया था। इस बार उसने पूछा-‘‘बाबू जी चाय ले आऊँ ?’ अचानक के इस प्रश्न से मेरे मस्तक पर दस्तक देते हुए बड़े-बड़े सवालों का हाथ रुक गया।
भारी कदमों से मैं उठा। नारे अब भी लग रहे थे, मांगें अभी भी रखी जा रही थीं, किसी यूनियन नेता का भाषण अब भी चल रहा था।
कार्यालयी-संस्कृति के विशद् इंद्रजाल से मोहित समाज की विवशता अनेक लेखकों और कहानीकारों की लेखनी का विषय रही है और कथाकारों ने व्यापक फलक पर इस संस्कृति के सच्चे व यथार्थ चित्र उकेरे हैं जिनमें नैतिक मूल्यों के ह्रास का रूपांकन करते समय उन्होंने कार्यालयी वास्तविकता के रंगों को अधिक-से-अधिक गहरा करने का प्रयास किया है।
इस संग्रह में कुछ ऐसे ही विशिष्ट कथाचित्र संगृहीत हैं।
सिफारिश
आज फिर एक ‘वेकेंसी’ मुझे अपने मतलब की नजर आती
है....आयु, अनुभव, अनिवार्य और वांछित योग्यताएं, तकरीबन सभी मेरे पास
हैं....सबसे बड़ी बात-सरकारी नौकरी। वैसे नौकरी तो मैं अभी भी कर रही हूं,
लेकिन एक प्राइवेट संस्थान में...जहां हर पल नौकरी जाने की आशंका बनी रहती
है। नौकरी जाने की क्या बात, मैंने खुद इसी तरह की चार नौकरियां छोड़कर यह
पांचवी की है। कारण ? कारण क्या-वही जो सब जानते
हैं-‘अप्वाइंटमेंट लेटर’ में सेवा की शर्तें जो भी
लिखीं हों, लेकिन जिस तरह की सेवा मालिक लोग महिला कर्मचारयों से लेते
रहते हैं या लेना चाहते हैं, उसका उसमें कोई जिक्र नहीं रहता। जो सेवा
करती हैं, मेवा पाती हैं, और यदि नहीं तो छुट्टी ! विशेष रूप से, अगर
सरपरस्तों को यह मालूम हो जाए कि महिला अकेली रहती है, तो बस, फिर तो
सहानुभूति-प्रक्षेपण का वह फार्मूला चलाते हैं जो अच्छी-अच्छी समझदारों को
भी धराशायीं कर देता है।...और फिर देखिए, उनके ठाठ, वेतन कुल जमा चार सौ
रुपये, लेकिन शरीर पर फ्रेंचशिफान से लेकर ‘इंटिमेट’
का मादक स्प्रे, टैक्सी से आना-जाना, घरों पर फ्रिज से लेकर टी.वी. तक का
होना...वगैरह-वगैरह !
यह बात नहीं कि मुझे इन सब चीजों की कसक सोने न देती हो।...लेकिन हां, इतना तो होता है कि सात घंटे ईमानदारी से काम करने के बाद भी जब झिड़िकियां खाने को मिलें, तब मन छोटा होता ही है, अजीब तरह का ‘कांप्लेक्स’ घर करने लगता है !
बचपन में ही पिता जी के न रहने से मां ने मुझे पाला-पोसा। कस्बे की कन्या-पाठशाला में पढ़ाते-पढ़ाते ही वह बेचारी बूढ़ी हो गई थीं। मेरे थोड़ा-सा समझदार हो जाने के साथ ही हम दोनों में अच्छी सहेलियों का-सा रिश्ता बन गया था। बचपन में पड़ोस के जिन लड़के-लड़कियों के साथ मैं खेलती-कूदती रही थी, वे भी अब मेरी ही तरह बड़े हो गए थे...लेकिन मां ने मेरी लड़कों से मैत्री का विरोध नहीं किया, हां, समय-समय पर जो बात उसे ठीक न लगती, उसे वह बड़े अच्छे उदाहरण देकर मुझे समझा देतीं।
मुझे याद है-पंद्रह की उम्र में जब पहली बार मुझे ‘कुछ’ हो गया था और मैं बुरी तरह घबरा गई थी तो मां ने समझाते हुए कहा था, ‘‘यह तो प्रकृति है गुड्डी, अब तुम लड़की से औरत बनने जा रही हो...इसी के बाद से औरत में मां बनने की क्षमता आ जाती है...इसलिए अब से लड़कों से ऐसे मेलजोल रखना चाहिए कि कोई ऊँच-नीच न हो।’’ इस तरह की ‘ऊंच-नीच’ का उपदेश मां प्रायः देती ही रहती थीं, जिसके कारण ‘चरित्र’, ‘नैतिकता’, ‘आचरण, जैसे कितने ही शब्द मेरे शब्दकोश में मोटे अक्षरों में लिख गए थे। एक बार मां नहीं थीं, हमेशा की तरह मेरा कभी का बालमित्र और अब का फर्स्ट-इयर में पढ़ने-वाला किशोर चन्ना घर आया था-मेरी मंगाई एक किताब लेकर। खाटपर बैठ मैंने जैसे ही उस किताब के पन्ने पलटने शुरू किए तो जिस्म में खून तेजी से सुनसुनाने लगा और किताब दूर फेंककर मैं झटके-से उठकर खड़ी हो गई। चन्ना ने मुझे कसकर बांहों में भरकर चूमना चाहा, लेकिन मैंने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उसे परे धकेल दिया और दरवाजा खोलकर बाहर बरामदे में हांफती-सी खड़ी हो गई। चन्ना बिना कुछ बोले चला गया था। इस घटना के बाद लड़कों और फिर धीरे-धीरे मर्दों की आंखें पढ़ने में माहिर होती गई थीं...ऐसा लगता, जैसे वे आंखें अपनी एक्सरे की-सी दृष्टि से भीतर के जिस्म का रेशा-रेशा उभारने की कोशिश करती हों। लेकिन धुर बचपन से मन में जमे मां के आदेश, उपदेशों की जड़ें काफी मजबूत होने से शाखें व पत्ते हिलडुल जाने के बावजूद जड़ों की पकड़ ढीली नहीं पड़ती थी।
इंटरमीडिएट तक की शिक्षा कस्बे की कन्या-पाठशाला में पूरी करने के बाद चालीस किलोमीटर दूर स्थित नगर के डिग्री कॉलेज में मुझे दाखिला दिलवाया गया। रोजाना बस से आना-जाना होता था। उस रेलमपेल में खुद को भरसक बचाए जाने के बाद भी कुछ-न-कुछ होता ही रहता था। मन तो होता कि उसी समय कालर पकड़कर एक तमाचा जड़ दूं, लेकिन जानती थी कि इस सबके बाद मेरी आगे की पढ़ाई निश्चय ही बंद कर दी जाएगी। मैं तब अजीब-सी लिजलिजी अनुभूति से भर उठती, जब देखती कि ऐसी हरकतें करने वाले युवक कम और प्रौढ़ या प्रौढ़ावस्था को लांघ जानेवाले वह थुलथुले पुरुष ही अधिक होते हैं जो इस तरह की हरकतों से अपने रोटी-दालनुमा दाम्पत्य-जीवन में देसी घी का बघार देना चाहते हों...। छिः यह सब सोचकर ही बस, की खिड़की में से सिर निकालकर उल्टी करने का मन होता था मेरा।
फिर बी.ए. का इम्ताहन देने के बाद गर्मी की दोपहरी में एक उल्टी के साथ ही पंखे-सी हो आई मां ने जब प्राण त्याग दिए, तब मेरी अकेली जिंदगी दोपहर के सूरज में तपती ताजा कोलतार बिछी उस सूनी सड़क-सी हो आई थी, जिस पर पांव जलते भी हों और चिपकते भी हों।
पहली नौकरी मुझे मां की जगह पर ही मिल गई थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद ‘बेटी’ कहनेवाले वहां के सफेद बालों वाले मैनेजर ने जब एक शाम सहानुभूति में सिर व पीठ पर हाथ फेरते-फेरते अंगुलियां कहीं और फिसलानी चाहीं, तब मुझसे एक पल भी वहां न रुका गया...और अगली नौकरी शहर में मिलने के साथ ही कस्बे का पुराना घर भी मुझसे छूट गया। लेकिन न दूसरी नौकरी रही, न तीसरी। एक ही बात को बार-बार अगर बताने बैठ गई तो आपको लगेगा जैसे किसी भी गली से जाने पर भी पहुंचना एक मकान को ही है...खैर, तो यह स्पष्ट कर ही दूं कि अभी तक की सभी नौकरियां प्राइवेट-स्कूल या दफ्तरों की ही थीं। चौथी नौकरी भी प्राइवेट ही थी, किंतु वहां मेरा मन रमने लगा था। क्योंकि मालिक, एक बहुत ही सुंदर, ताजा-ताजा विदेश से पढ़ाई पूरी करके आया नवयुवक था-बहुत विनम्र और शिष्ट। निगाह मिलाकर तो कभी बात नहीं करता था। उसकी इन्ही अदाओं ने दफ्तर की लड़कियों के मन में उसके लिए खासा ‘क्रैज’ जगा दिया था। उसके कमरे में जाने के लिए वह बहाने टटोला करतीं और जाने से पहले ‘मेकअप’ को दुरुस्त करना न भूलतीं।
एक बार नववर्ष की शुभकामनाएँ देने हम सभी लड़कियां एक साथ साहब के चैंबर में गईं। मुझे लगा जैसे इस सामूहिक धावे से साहब असहज से हो आए थे। शुभकामनाओं का जवाब देने के साथ ही उन्होंने सभी पर सरसरी दृष्टि डाली, मुझसे दृष्टि मिलते ही उन्होंने पूछा कि क्या मैं नयी आई हूं ! मैंने बताया कि आए हुए तो कुछ महीने हो गए हैं, किन्तु उनके चैम्बर में आने का यह पहला ही अवसर है। हम लोग जब बाहर आ रहे थे, तब उन्होंने क्षमा मांगते मेरा नाम भी पूछा था और मेरे बताने पर शायद धीरे-से उसे दोहराया भी था ‘रुचि’...इतने सालों में पहली बार मैंने भी कुछ महसूस किया था। मुझे सब कुछ अच्छा भी लगा था, और उसके बाद से मैं अपनी ओर जागरूक भी हो आई थी। साहब अक्सर मुझे किसी न किसी फाइल के साथ बुलवाते रहते और जाने के बाद कॉफी पिए बिना कतई न आने देते। ईर्ष्यालु लड़कियों की दृष्टियों से बिंधते रहने के बावजूद मैं दिनों-दिन जैसे ‘बोल्ड’ होती जा रही थी। हम दफ्तर के बाद बाहर भी शामें गुजारने लगे थे। इतना ही नहीं, अपने एकाकी-जीवन की व्यथा-कथा सुना-सुनाकर उन्होंने मेरी सहानुभूति भी किसी सीमा तक पा ली थी। मन में ऐसा प्यार उमड़ता कि क्या न कर दूं इस इंसान के लिए...और एक रोज कॉफी-हाउस’ के केबिन के झुटपुटे में मुझे प्यार करते...उफनती सांसों पर काबू पाते हुए उन्होंने कहा कि वह अपनी पूरी-की-पूरी जिंदगी मेरे हाथों सौंप देना चाहते हैं....सुनकर मेरे कानों में जैसे घंटियां-सी बज उठी थीं, नशे की-सी स्थिति में उनके कंधे पर अपना सिर टिकाकर जैसे मैंने अपनी सहज स्वीकृति दे डाली थी। अलग होने से पहले आंखों-में-आंखों पिरोकर गहरी दृष्टि से देखते हुए उन्होंने साधिकार कहा, ‘‘कल हम घर पर मिल रहे हैं...मेरे घर पर...’’शरारत से मैंने कहा, ‘‘...और मेरा घर नहीं...’’ठहाका लगाते हुए वह बोले, ‘‘पहले तुम्हारा...फिर मेरा।’’
यह बात नहीं कि मुझे इन सब चीजों की कसक सोने न देती हो।...लेकिन हां, इतना तो होता है कि सात घंटे ईमानदारी से काम करने के बाद भी जब झिड़िकियां खाने को मिलें, तब मन छोटा होता ही है, अजीब तरह का ‘कांप्लेक्स’ घर करने लगता है !
बचपन में ही पिता जी के न रहने से मां ने मुझे पाला-पोसा। कस्बे की कन्या-पाठशाला में पढ़ाते-पढ़ाते ही वह बेचारी बूढ़ी हो गई थीं। मेरे थोड़ा-सा समझदार हो जाने के साथ ही हम दोनों में अच्छी सहेलियों का-सा रिश्ता बन गया था। बचपन में पड़ोस के जिन लड़के-लड़कियों के साथ मैं खेलती-कूदती रही थी, वे भी अब मेरी ही तरह बड़े हो गए थे...लेकिन मां ने मेरी लड़कों से मैत्री का विरोध नहीं किया, हां, समय-समय पर जो बात उसे ठीक न लगती, उसे वह बड़े अच्छे उदाहरण देकर मुझे समझा देतीं।
मुझे याद है-पंद्रह की उम्र में जब पहली बार मुझे ‘कुछ’ हो गया था और मैं बुरी तरह घबरा गई थी तो मां ने समझाते हुए कहा था, ‘‘यह तो प्रकृति है गुड्डी, अब तुम लड़की से औरत बनने जा रही हो...इसी के बाद से औरत में मां बनने की क्षमता आ जाती है...इसलिए अब से लड़कों से ऐसे मेलजोल रखना चाहिए कि कोई ऊँच-नीच न हो।’’ इस तरह की ‘ऊंच-नीच’ का उपदेश मां प्रायः देती ही रहती थीं, जिसके कारण ‘चरित्र’, ‘नैतिकता’, ‘आचरण, जैसे कितने ही शब्द मेरे शब्दकोश में मोटे अक्षरों में लिख गए थे। एक बार मां नहीं थीं, हमेशा की तरह मेरा कभी का बालमित्र और अब का फर्स्ट-इयर में पढ़ने-वाला किशोर चन्ना घर आया था-मेरी मंगाई एक किताब लेकर। खाटपर बैठ मैंने जैसे ही उस किताब के पन्ने पलटने शुरू किए तो जिस्म में खून तेजी से सुनसुनाने लगा और किताब दूर फेंककर मैं झटके-से उठकर खड़ी हो गई। चन्ना ने मुझे कसकर बांहों में भरकर चूमना चाहा, लेकिन मैंने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उसे परे धकेल दिया और दरवाजा खोलकर बाहर बरामदे में हांफती-सी खड़ी हो गई। चन्ना बिना कुछ बोले चला गया था। इस घटना के बाद लड़कों और फिर धीरे-धीरे मर्दों की आंखें पढ़ने में माहिर होती गई थीं...ऐसा लगता, जैसे वे आंखें अपनी एक्सरे की-सी दृष्टि से भीतर के जिस्म का रेशा-रेशा उभारने की कोशिश करती हों। लेकिन धुर बचपन से मन में जमे मां के आदेश, उपदेशों की जड़ें काफी मजबूत होने से शाखें व पत्ते हिलडुल जाने के बावजूद जड़ों की पकड़ ढीली नहीं पड़ती थी।
इंटरमीडिएट तक की शिक्षा कस्बे की कन्या-पाठशाला में पूरी करने के बाद चालीस किलोमीटर दूर स्थित नगर के डिग्री कॉलेज में मुझे दाखिला दिलवाया गया। रोजाना बस से आना-जाना होता था। उस रेलमपेल में खुद को भरसक बचाए जाने के बाद भी कुछ-न-कुछ होता ही रहता था। मन तो होता कि उसी समय कालर पकड़कर एक तमाचा जड़ दूं, लेकिन जानती थी कि इस सबके बाद मेरी आगे की पढ़ाई निश्चय ही बंद कर दी जाएगी। मैं तब अजीब-सी लिजलिजी अनुभूति से भर उठती, जब देखती कि ऐसी हरकतें करने वाले युवक कम और प्रौढ़ या प्रौढ़ावस्था को लांघ जानेवाले वह थुलथुले पुरुष ही अधिक होते हैं जो इस तरह की हरकतों से अपने रोटी-दालनुमा दाम्पत्य-जीवन में देसी घी का बघार देना चाहते हों...। छिः यह सब सोचकर ही बस, की खिड़की में से सिर निकालकर उल्टी करने का मन होता था मेरा।
फिर बी.ए. का इम्ताहन देने के बाद गर्मी की दोपहरी में एक उल्टी के साथ ही पंखे-सी हो आई मां ने जब प्राण त्याग दिए, तब मेरी अकेली जिंदगी दोपहर के सूरज में तपती ताजा कोलतार बिछी उस सूनी सड़क-सी हो आई थी, जिस पर पांव जलते भी हों और चिपकते भी हों।
पहली नौकरी मुझे मां की जगह पर ही मिल गई थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद ‘बेटी’ कहनेवाले वहां के सफेद बालों वाले मैनेजर ने जब एक शाम सहानुभूति में सिर व पीठ पर हाथ फेरते-फेरते अंगुलियां कहीं और फिसलानी चाहीं, तब मुझसे एक पल भी वहां न रुका गया...और अगली नौकरी शहर में मिलने के साथ ही कस्बे का पुराना घर भी मुझसे छूट गया। लेकिन न दूसरी नौकरी रही, न तीसरी। एक ही बात को बार-बार अगर बताने बैठ गई तो आपको लगेगा जैसे किसी भी गली से जाने पर भी पहुंचना एक मकान को ही है...खैर, तो यह स्पष्ट कर ही दूं कि अभी तक की सभी नौकरियां प्राइवेट-स्कूल या दफ्तरों की ही थीं। चौथी नौकरी भी प्राइवेट ही थी, किंतु वहां मेरा मन रमने लगा था। क्योंकि मालिक, एक बहुत ही सुंदर, ताजा-ताजा विदेश से पढ़ाई पूरी करके आया नवयुवक था-बहुत विनम्र और शिष्ट। निगाह मिलाकर तो कभी बात नहीं करता था। उसकी इन्ही अदाओं ने दफ्तर की लड़कियों के मन में उसके लिए खासा ‘क्रैज’ जगा दिया था। उसके कमरे में जाने के लिए वह बहाने टटोला करतीं और जाने से पहले ‘मेकअप’ को दुरुस्त करना न भूलतीं।
एक बार नववर्ष की शुभकामनाएँ देने हम सभी लड़कियां एक साथ साहब के चैंबर में गईं। मुझे लगा जैसे इस सामूहिक धावे से साहब असहज से हो आए थे। शुभकामनाओं का जवाब देने के साथ ही उन्होंने सभी पर सरसरी दृष्टि डाली, मुझसे दृष्टि मिलते ही उन्होंने पूछा कि क्या मैं नयी आई हूं ! मैंने बताया कि आए हुए तो कुछ महीने हो गए हैं, किन्तु उनके चैम्बर में आने का यह पहला ही अवसर है। हम लोग जब बाहर आ रहे थे, तब उन्होंने क्षमा मांगते मेरा नाम भी पूछा था और मेरे बताने पर शायद धीरे-से उसे दोहराया भी था ‘रुचि’...इतने सालों में पहली बार मैंने भी कुछ महसूस किया था। मुझे सब कुछ अच्छा भी लगा था, और उसके बाद से मैं अपनी ओर जागरूक भी हो आई थी। साहब अक्सर मुझे किसी न किसी फाइल के साथ बुलवाते रहते और जाने के बाद कॉफी पिए बिना कतई न आने देते। ईर्ष्यालु लड़कियों की दृष्टियों से बिंधते रहने के बावजूद मैं दिनों-दिन जैसे ‘बोल्ड’ होती जा रही थी। हम दफ्तर के बाद बाहर भी शामें गुजारने लगे थे। इतना ही नहीं, अपने एकाकी-जीवन की व्यथा-कथा सुना-सुनाकर उन्होंने मेरी सहानुभूति भी किसी सीमा तक पा ली थी। मन में ऐसा प्यार उमड़ता कि क्या न कर दूं इस इंसान के लिए...और एक रोज कॉफी-हाउस’ के केबिन के झुटपुटे में मुझे प्यार करते...उफनती सांसों पर काबू पाते हुए उन्होंने कहा कि वह अपनी पूरी-की-पूरी जिंदगी मेरे हाथों सौंप देना चाहते हैं....सुनकर मेरे कानों में जैसे घंटियां-सी बज उठी थीं, नशे की-सी स्थिति में उनके कंधे पर अपना सिर टिकाकर जैसे मैंने अपनी सहज स्वीकृति दे डाली थी। अलग होने से पहले आंखों-में-आंखों पिरोकर गहरी दृष्टि से देखते हुए उन्होंने साधिकार कहा, ‘‘कल हम घर पर मिल रहे हैं...मेरे घर पर...’’शरारत से मैंने कहा, ‘‘...और मेरा घर नहीं...’’ठहाका लगाते हुए वह बोले, ‘‘पहले तुम्हारा...फिर मेरा।’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book