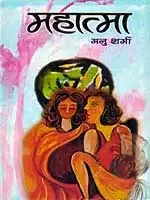|
कहानी संग्रह >> महात्मा महात्मामनु शर्मा
|
177 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है श्रेष्ठ कहानी संग्रह...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
ये कहानियाँ मेरे उपन्यासों के अंतराल की उत्पाद हैं; पर ये उपन्यास नहीं
हैं-न आकार में और न प्रकार में। यद्यपि आज भी यह बात उठ रही है कि कहानी
कोई विधा ही नहीं है। जो कुछ है वह उपन्यास ही है। आकार की लघुता में भी
वह उपन्यास है—और विशालता में तो है ही। दोनों में कथा-शिल्प एक
है।
मेरा ‘पात्र’ जिन ऊबड़-खाबड़ पगडंडियों पर ले चलता है वहाँ मैं अकेला नहीं होता। एक तो मेरा विवेक मेरे साथ होता है और दूसरे, मेरी कल्पना मेरे साथ होती है। विवेक रेखांकन करता है और कल्पना रंग भरती है। रेखांकन के बाहर उसका रंग नहीं जाता। विवेक कल्पना का नियन्त्रण है, ‘‘पकड़’ है। जब कल्पना रेखांकन के बाहर जाने लगती है या वायवी होने लगती है तब विवेक कहता है, ‘ठहरो, कुछ सोच-विचार करो।’....और बाहर जाने की अपनी प्रकृति के बावजूद वह यथार्थ के दायरे में ही रहती है। तब वे चित्र बनते हैं, जिनके कुछ नमूने इस संग्रह में हैं।
मेरा ‘पात्र’ जिन ऊबड़-खाबड़ पगडंडियों पर ले चलता है वहाँ मैं अकेला नहीं होता। एक तो मेरा विवेक मेरे साथ होता है और दूसरे, मेरी कल्पना मेरे साथ होती है। विवेक रेखांकन करता है और कल्पना रंग भरती है। रेखांकन के बाहर उसका रंग नहीं जाता। विवेक कल्पना का नियन्त्रण है, ‘‘पकड़’ है। जब कल्पना रेखांकन के बाहर जाने लगती है या वायवी होने लगती है तब विवेक कहता है, ‘ठहरो, कुछ सोच-विचार करो।’....और बाहर जाने की अपनी प्रकृति के बावजूद वह यथार्थ के दायरे में ही रहती है। तब वे चित्र बनते हैं, जिनके कुछ नमूने इस संग्रह में हैं।
लेखक
कहानियाँ लिखते हुए
मैं कहानियाँ क्यों लिखता हूँ ? आप यकीन मानिए, आज तक मेरे पास इस प्रश्न
का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। यात्रा और बीमारी के दिनों को छोड़कर, लगभग
नियमित रूप से, प्रायः प्रतिदिन मैं ठीक समय से अपनी राइटिंग टेबल पर आकर
बैठ जाता हूँ— एकदम कोरा, सादा और खाली। जैसे कोई खाली घड़ा
बहते
बंबे के नीचे आ जाए और वह भरने लगे। यह स्थित बहुत समय तक नहीं होती।
कभी-कभी कुछ ही समय में घड़ा भर जाता है और कभी घंटों लग जाते हैं। इस बीच
चिंतन की जिन तहों और मन की जिन अनुभूतियों से गुजरता हूँ, उनके बारे में
कुछ कह पाना मेरे लिए संभव नहीं है। यही समझिए कि बंद बड़े कमरे के अँधेरे
में मैं या मेरी कल्पना कुछ टटोलती है और सौभाग्य से कभी खाली हाथ नहीं
लौटती। कुछ-न-कुछ हाथ लग ही जाता है—कोई चरित्र, कोई घटना या
दुर्घटना।
इनमें ऐसी भी घटनाएँ हो सकती हैं, जो अभी घटी नहीं होती हैं या घटते हुए स्वंय को अधूरा ही छोड़ जाती हैं।
यह सब कुछ उसी संसार और उसी समाज का होता है, जिसमें मैं साँस लेता हूँ; फिर भी यह मेरा भोगा यथार्थ नहीं है। आखिर एक आदमी संसार के कितने यथार्थ भोग सकता है ? शायद उसे कई जन्म लेने पड़ें, तब भी उसका यह सपना पूरा न होगा। फिर भी मैं इसे सिरे से नकार नहीं सकता कि इन कहानियों में वर्णित यथार्थ को मैंने भोगा नहीं है। हाँ, यह अवश्य है कि इनमें से कुछ यथार्थ को मैंने जीया है, कुछ को भर आँखों पीया है, कुछ को सुना है, कुछ को गुना है और कुछ को मेरी कल्पना ने बुना है।
जब मैं उस अँधेरे बँद कमरे से कुछ लेकर निकलता हूँ तो बहुधा स्वयं को उसके प्रति पूर्ण समर्पित कर देता हूँ, जैसे शव पूर्ण रूप से धारा के हवाले कर दिया जाता है; बिना किसी प्रतिरोध या बचाव की चिंता के मैं भी धारा का हो जाता हूँ। पर उसमें और मुझमें अंतर है। वह शव है और मैं शिव हूँ, शक्ति के साथ हूँ। मेरी शक्ति मेरी जीवंतता है, जिसमें विवेक है, बुद्धि है, जो मुझे स्वयं मेरे ‘होने’ का बोध कराती है।
बस उसी धारा के दिए ‘चरित्र’ के कंधे पर हाथ रखकर, उसी के सहारे चलता हूँ; पर आँखें बंद कर नहीं—खुली आँखों से, पूरी सजगता के साथ, घाट-घाट का पानी पीता हुआ, कड़वे–मीठे अनुभव समेटता हुआ।
फिर उसी चरित्र का भोगा, मेरा भोगा हो जाता ही, उसी का देखा मेरा देखा हो जाता है और उसी का कहा मेरा कहा। दरअसल वह आवाज भी उसी की आवाज होती है, जो मेरी कलम से निकलती है। इस संदर्भ में मैं प्रेमचंदजी के साथ हो लेता हूँ, कि मैं तो नदी के किनारे का नरकुल हूँ। मेरी आवाज उन हवाओं की आवाज है, जो मुझसे होकर गुजरती हैं।’
मेरा ‘पात्र’ जिन ऊबड़-खाबड़ पगडंडियों पर ले चलता है वहाँ मैं अकेला नहीं होता। एक तो मेरा विवेक मेरे साथ होता है, और दूसरी मेरी कल्पना मेरे साथ होती है। विवेक रेखांकन करता है और कल्पना रंग भरती है। रेखांकन के बाहर उसका रंग नहीं जाता। विवेक कल्पना का नियंत्रण है, ‘‘पकड़’ है। जब कल्पना रेखांकन के बाहर जाने लगती है या वायवी होने लगती है तब विवेक कहता है, ‘ठहरो, कुछ सोच-विचार करो।’....और बाहर जाने की अपनी प्रकृति के बावजूद वह यथार्थ के दायरे में ही रहती है। तब वे चित्र बनते हैं, जिनके कुछ नमूने इस संग्रह में हैं।
ये कहानियाँ मेरे उपन्यासों के अंतराल की उत्पाद हैं; पर ये उपन्यास नहीं हैं—न आकार में और न प्रकार में। यद्यपि आज यह बात भी उठ रही है कि ‘कहानी कोई विधा नहीं है। जो कुछ है वह उपन्यास ही है। आकार की लघुता में भी वह उपन्यास है—और विशालता में तो है ही। दोनों में कथा-शिल्प एक है। ये विचार अभी-अभी जर्मनी में संपन्न हुए उपन्यासकारों के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उठे; पर वे लोग भी किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुँच सके। मेरे विचार तो दोनों की नस्ल भले ही एक हो, पर जाति और प्रजाति अलग है, प्रकृति अलग है; दोनों की प्रभावान्विक्तयों के स्तर अलग हैं और उनके घनत्व में भी भिन्नता है।’
यह भी आवाज उठी कि कहानी मर चुकी है, या मर रही है। यदि वह मर गयी तो कहानी कैसी ? हम रहें या न रहें, पर हमारी कहानी तो रहेगी ही। कहानी और कविता जितने आंदोलनों से गुजरी है उतनी शायद हिंदी की कोई और विधा नहीं। इस आंदोलन ने कहानी का रूप तो उतना नहीं सँवारा जितना उसे नाम दिया। कहानी कई संज्ञाओं से विभूषित हुई—कहानी, नई कहानी, साठोत्तरी कहानी, अकहानी, सचेतक कहानी, आम आदमी की कहानी, समानांतर कहानी आदि। पर कहानी की अनिवार्यता थी हर नाम में। केवल विशेषण बदलते गए। संज्ञा ज्यों-की-त्यों रही। एक-से-एक नए घाट बनते रहे, पर धारा एक थी। यह जरूर हुआ कि वह कहीं पतली हुई, कहीं फैली, कहीं गहरी और कहीं उथली। धारा का सूखना कहानी की मौत होती है। पर कभी मरी नहीं और न धारा सूखी। एक आवाज एक झटके से उठी और ऊपर से निकल गई कि कविता मर गई, कहानी मर रही है। पश्चिम से उठी यह आवाज कविता के संबंध में अधिक जोरदार थी।
जिन लोगों ने कहानी की मौत की बात उठाई, शायद उनके विचार की अँगुलियाँ कहानी की नब्ज पर नहीं थीं। वे उसकी धड़कन को पहचान न सके। कभी-कभी ऐसा होता है कि धड़कन इतनी मंद और मंथर हो जाती है कि बड़े-बड़े चिकित्सकों की गिरफ्त में नहीं आती; पर होती अवश्य है, वरना जीवन कैसे होता ?
कहानी का जीवन बना रहा, वह आंदोलन से गुजरती रही। इन आन्दोलनों ने उसे झकझोरा, उसके लिए खतरा उत्पन्न किया। फिर भी कहानी उन खतरों से निकलती गई और आंदोलन अपनी प्रकृति के अनुसार ज्वार की तरह उठते रहे और भाटे की तरह उतरते चले गए। वे उसके अस्तित्व को हिला न सके। उसकी अस्मिता अडिग रही। आखिर कहानी की यह अस्मिता है क्या ?’ क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी ?’ इस संदर्भ में एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ।
सुना है, एक बार सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा कोई ऐसी कहानी सुनाओ, जो खत्म होने वाली न हो। शायद वह रात बिताने के लिए उससे अलिफ-लैला कहानी सुनना चाहता था; पर बीरबल ने दूसरा ही रास्ता पकड़ा। उसने कहानी सुनानी आरंभ की, ‘एक किसान था। उसने अपने खेत में गेहूँ बोया। एक दाना बोया, दो दाने बोए, तीन दाने बोए....।’ ऐसा ही वह बहुत देर तक गिनता चला गया। अंत में झुँझलाकर अकबर ने कहा, ‘सुन लिया उसने गेहूँ बोया। फिर क्या हुआ ?’
‘फिर वर्षा ऋतु आई। आसमान पर बादल छाने लगे। एक बादल आया, दूसरा बादल आया, तीसरा बादल आया...।’
फिर सम्राट झल्लाया, ‘अरे, सुन लिया कि बादल आ गए, वर्षा हुई। फिर क्या हुआ ?...
‘फिर क्या, हुजूर, कि गेहूँ उगा। एक अंकुर फूटा, दो अंकुर फूटे, तीन अंकुर फूटे...।’ उसने फिर अपना पुराना ढर्रा अख्तियार किया।
अकबर फिर झुँझलाया, ‘यह क्या कर रहे हो ?’
‘हुजूर, कहानी सुना रहा हूँ। जितने अँकुर उगे अलग-अलग बतला रहा हूँ।’ अकबर ने खीझकर कहानी बंद करा दी, क्योंकि वह कहानी ही नहीं थी। उसमें ‘क्या हुआ’ को शांत करने की शक्ति नहीं थी। उसमें ‘एलिमेंट ऑफ सस्पेंस’ नहीं था, कुतूहल की वृत्ति नहीं थी। यही कुतूहल की वृत्ति कहानी की अस्मिता है, कहानी की आत्मा है।
यह सत्य है कि बिना शरीर के आत्मा का प्रकाश संभव नहीं। वैसे ही कहानी के अन्य तत्त्व उसके शरीर के एक-एक अंग हैं, इंद्रिय हैं। भले ही वह शरीर आदमी का न होकर कीड़े-मकोड़े का ही क्यों न हो।
कहानी अपने आदि रूप में ‘कुतूहल की वृति’ ही लेकर आई थी। चाहे वह सत्य हरिश्चंद्र की कहानी हो या ‘राय गुलबकावली’ की या शीत वसंत की। उस समय कहानी के और तत्त्व बड़े भी थे। भोगे हुए यथार्थ का दूर-दूर तक अता-पता नहीं था। भले ही वह ‘नानी की कहानी’ ही क्यों न रही हो। उसी के सहारे नानी अपने नाती-नातिनों को सुलाती रही और उसकी मंगल कामना इस निष्कर्ष पर आती रही, ‘जैसै उस राजा के दिन लौटे वैसे सबके दिन लौटें।’’
कहानी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती गई, उसके अन्य तत्त्व विकसित होते गए; जैसे-वातावरण, चरित्र-चित्रण, उद्देश्य आदि-आदि। कहानी परियों के लोक से धरती पर आई। उसे माटी की गंध मिली 4, आदमी का संस्पर्श मिला; आम आदमी की संवेदनशीलता उसकी संवेदना बनी। फिर उसने जमीन की तलाश की।
हमारे जीवन के आदर्श को पकड़े हुए वह यथार्थ की ओर बढ़ी और अंत में यथार्थ का ही आदर्श उसके हाथ रह गया। यह यथार्थ खुद का ‘भोगा हुआ के नाम पर देखा, सुना और गुना अधिक रह गया।’
कहानी की इस विकास-यात्रा में कुतूहल का तत्त्व झीना होता गया और अंत में आते-आते आज की कहानियों में वह अदृश्य की सीमा तक ही दृश्य रह गया। कहानी सपाट होती गई और उसकी पठनीतया दुर्बल। जिन कहानीकारों मे उसकी पठनीयता का ध्यान रखा उन्हें ‘किस्सागो’ कहा गया और उसे कहानी के राज्य का द्वितीय श्रेणी का नगरिक माना गया। प्रथम श्रेणी के नागरिक को ‘अफसाना निगार’ कहा गया। मैं नहीं जानता कि मैं कहानी के राजेय का किस श्रेणी का नागरिक हूँ—और हूँ भी कि नहीं हूँ ! इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ।
इनमें ऐसी भी घटनाएँ हो सकती हैं, जो अभी घटी नहीं होती हैं या घटते हुए स्वंय को अधूरा ही छोड़ जाती हैं।
यह सब कुछ उसी संसार और उसी समाज का होता है, जिसमें मैं साँस लेता हूँ; फिर भी यह मेरा भोगा यथार्थ नहीं है। आखिर एक आदमी संसार के कितने यथार्थ भोग सकता है ? शायद उसे कई जन्म लेने पड़ें, तब भी उसका यह सपना पूरा न होगा। फिर भी मैं इसे सिरे से नकार नहीं सकता कि इन कहानियों में वर्णित यथार्थ को मैंने भोगा नहीं है। हाँ, यह अवश्य है कि इनमें से कुछ यथार्थ को मैंने जीया है, कुछ को भर आँखों पीया है, कुछ को सुना है, कुछ को गुना है और कुछ को मेरी कल्पना ने बुना है।
जब मैं उस अँधेरे बँद कमरे से कुछ लेकर निकलता हूँ तो बहुधा स्वयं को उसके प्रति पूर्ण समर्पित कर देता हूँ, जैसे शव पूर्ण रूप से धारा के हवाले कर दिया जाता है; बिना किसी प्रतिरोध या बचाव की चिंता के मैं भी धारा का हो जाता हूँ। पर उसमें और मुझमें अंतर है। वह शव है और मैं शिव हूँ, शक्ति के साथ हूँ। मेरी शक्ति मेरी जीवंतता है, जिसमें विवेक है, बुद्धि है, जो मुझे स्वयं मेरे ‘होने’ का बोध कराती है।
बस उसी धारा के दिए ‘चरित्र’ के कंधे पर हाथ रखकर, उसी के सहारे चलता हूँ; पर आँखें बंद कर नहीं—खुली आँखों से, पूरी सजगता के साथ, घाट-घाट का पानी पीता हुआ, कड़वे–मीठे अनुभव समेटता हुआ।
फिर उसी चरित्र का भोगा, मेरा भोगा हो जाता ही, उसी का देखा मेरा देखा हो जाता है और उसी का कहा मेरा कहा। दरअसल वह आवाज भी उसी की आवाज होती है, जो मेरी कलम से निकलती है। इस संदर्भ में मैं प्रेमचंदजी के साथ हो लेता हूँ, कि मैं तो नदी के किनारे का नरकुल हूँ। मेरी आवाज उन हवाओं की आवाज है, जो मुझसे होकर गुजरती हैं।’
मेरा ‘पात्र’ जिन ऊबड़-खाबड़ पगडंडियों पर ले चलता है वहाँ मैं अकेला नहीं होता। एक तो मेरा विवेक मेरे साथ होता है, और दूसरी मेरी कल्पना मेरे साथ होती है। विवेक रेखांकन करता है और कल्पना रंग भरती है। रेखांकन के बाहर उसका रंग नहीं जाता। विवेक कल्पना का नियंत्रण है, ‘‘पकड़’ है। जब कल्पना रेखांकन के बाहर जाने लगती है या वायवी होने लगती है तब विवेक कहता है, ‘ठहरो, कुछ सोच-विचार करो।’....और बाहर जाने की अपनी प्रकृति के बावजूद वह यथार्थ के दायरे में ही रहती है। तब वे चित्र बनते हैं, जिनके कुछ नमूने इस संग्रह में हैं।
ये कहानियाँ मेरे उपन्यासों के अंतराल की उत्पाद हैं; पर ये उपन्यास नहीं हैं—न आकार में और न प्रकार में। यद्यपि आज यह बात भी उठ रही है कि ‘कहानी कोई विधा नहीं है। जो कुछ है वह उपन्यास ही है। आकार की लघुता में भी वह उपन्यास है—और विशालता में तो है ही। दोनों में कथा-शिल्प एक है। ये विचार अभी-अभी जर्मनी में संपन्न हुए उपन्यासकारों के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उठे; पर वे लोग भी किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुँच सके। मेरे विचार तो दोनों की नस्ल भले ही एक हो, पर जाति और प्रजाति अलग है, प्रकृति अलग है; दोनों की प्रभावान्विक्तयों के स्तर अलग हैं और उनके घनत्व में भी भिन्नता है।’
यह भी आवाज उठी कि कहानी मर चुकी है, या मर रही है। यदि वह मर गयी तो कहानी कैसी ? हम रहें या न रहें, पर हमारी कहानी तो रहेगी ही। कहानी और कविता जितने आंदोलनों से गुजरी है उतनी शायद हिंदी की कोई और विधा नहीं। इस आंदोलन ने कहानी का रूप तो उतना नहीं सँवारा जितना उसे नाम दिया। कहानी कई संज्ञाओं से विभूषित हुई—कहानी, नई कहानी, साठोत्तरी कहानी, अकहानी, सचेतक कहानी, आम आदमी की कहानी, समानांतर कहानी आदि। पर कहानी की अनिवार्यता थी हर नाम में। केवल विशेषण बदलते गए। संज्ञा ज्यों-की-त्यों रही। एक-से-एक नए घाट बनते रहे, पर धारा एक थी। यह जरूर हुआ कि वह कहीं पतली हुई, कहीं फैली, कहीं गहरी और कहीं उथली। धारा का सूखना कहानी की मौत होती है। पर कभी मरी नहीं और न धारा सूखी। एक आवाज एक झटके से उठी और ऊपर से निकल गई कि कविता मर गई, कहानी मर रही है। पश्चिम से उठी यह आवाज कविता के संबंध में अधिक जोरदार थी।
जिन लोगों ने कहानी की मौत की बात उठाई, शायद उनके विचार की अँगुलियाँ कहानी की नब्ज पर नहीं थीं। वे उसकी धड़कन को पहचान न सके। कभी-कभी ऐसा होता है कि धड़कन इतनी मंद और मंथर हो जाती है कि बड़े-बड़े चिकित्सकों की गिरफ्त में नहीं आती; पर होती अवश्य है, वरना जीवन कैसे होता ?
कहानी का जीवन बना रहा, वह आंदोलन से गुजरती रही। इन आन्दोलनों ने उसे झकझोरा, उसके लिए खतरा उत्पन्न किया। फिर भी कहानी उन खतरों से निकलती गई और आंदोलन अपनी प्रकृति के अनुसार ज्वार की तरह उठते रहे और भाटे की तरह उतरते चले गए। वे उसके अस्तित्व को हिला न सके। उसकी अस्मिता अडिग रही। आखिर कहानी की यह अस्मिता है क्या ?’ क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी ?’ इस संदर्भ में एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ।
सुना है, एक बार सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा कोई ऐसी कहानी सुनाओ, जो खत्म होने वाली न हो। शायद वह रात बिताने के लिए उससे अलिफ-लैला कहानी सुनना चाहता था; पर बीरबल ने दूसरा ही रास्ता पकड़ा। उसने कहानी सुनानी आरंभ की, ‘एक किसान था। उसने अपने खेत में गेहूँ बोया। एक दाना बोया, दो दाने बोए, तीन दाने बोए....।’ ऐसा ही वह बहुत देर तक गिनता चला गया। अंत में झुँझलाकर अकबर ने कहा, ‘सुन लिया उसने गेहूँ बोया। फिर क्या हुआ ?’
‘फिर वर्षा ऋतु आई। आसमान पर बादल छाने लगे। एक बादल आया, दूसरा बादल आया, तीसरा बादल आया...।’
फिर सम्राट झल्लाया, ‘अरे, सुन लिया कि बादल आ गए, वर्षा हुई। फिर क्या हुआ ?...
‘फिर क्या, हुजूर, कि गेहूँ उगा। एक अंकुर फूटा, दो अंकुर फूटे, तीन अंकुर फूटे...।’ उसने फिर अपना पुराना ढर्रा अख्तियार किया।
अकबर फिर झुँझलाया, ‘यह क्या कर रहे हो ?’
‘हुजूर, कहानी सुना रहा हूँ। जितने अँकुर उगे अलग-अलग बतला रहा हूँ।’ अकबर ने खीझकर कहानी बंद करा दी, क्योंकि वह कहानी ही नहीं थी। उसमें ‘क्या हुआ’ को शांत करने की शक्ति नहीं थी। उसमें ‘एलिमेंट ऑफ सस्पेंस’ नहीं था, कुतूहल की वृत्ति नहीं थी। यही कुतूहल की वृत्ति कहानी की अस्मिता है, कहानी की आत्मा है।
यह सत्य है कि बिना शरीर के आत्मा का प्रकाश संभव नहीं। वैसे ही कहानी के अन्य तत्त्व उसके शरीर के एक-एक अंग हैं, इंद्रिय हैं। भले ही वह शरीर आदमी का न होकर कीड़े-मकोड़े का ही क्यों न हो।
कहानी अपने आदि रूप में ‘कुतूहल की वृति’ ही लेकर आई थी। चाहे वह सत्य हरिश्चंद्र की कहानी हो या ‘राय गुलबकावली’ की या शीत वसंत की। उस समय कहानी के और तत्त्व बड़े भी थे। भोगे हुए यथार्थ का दूर-दूर तक अता-पता नहीं था। भले ही वह ‘नानी की कहानी’ ही क्यों न रही हो। उसी के सहारे नानी अपने नाती-नातिनों को सुलाती रही और उसकी मंगल कामना इस निष्कर्ष पर आती रही, ‘जैसै उस राजा के दिन लौटे वैसे सबके दिन लौटें।’’
कहानी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती गई, उसके अन्य तत्त्व विकसित होते गए; जैसे-वातावरण, चरित्र-चित्रण, उद्देश्य आदि-आदि। कहानी परियों के लोक से धरती पर आई। उसे माटी की गंध मिली 4, आदमी का संस्पर्श मिला; आम आदमी की संवेदनशीलता उसकी संवेदना बनी। फिर उसने जमीन की तलाश की।
हमारे जीवन के आदर्श को पकड़े हुए वह यथार्थ की ओर बढ़ी और अंत में यथार्थ का ही आदर्श उसके हाथ रह गया। यह यथार्थ खुद का ‘भोगा हुआ के नाम पर देखा, सुना और गुना अधिक रह गया।’
कहानी की इस विकास-यात्रा में कुतूहल का तत्त्व झीना होता गया और अंत में आते-आते आज की कहानियों में वह अदृश्य की सीमा तक ही दृश्य रह गया। कहानी सपाट होती गई और उसकी पठनीतया दुर्बल। जिन कहानीकारों मे उसकी पठनीयता का ध्यान रखा उन्हें ‘किस्सागो’ कहा गया और उसे कहानी के राज्य का द्वितीय श्रेणी का नगरिक माना गया। प्रथम श्रेणी के नागरिक को ‘अफसाना निगार’ कहा गया। मैं नहीं जानता कि मैं कहानी के राजेय का किस श्रेणी का नागरिक हूँ—और हूँ भी कि नहीं हूँ ! इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ।
पुनश्च :
मैं इतना कृतघ्न नहीं कि ‘माया’ के पूर्व संपादक श्री
वशिष्ठ
मुनि ओझा के प्रति आभार न प्रदर्शित करूँ। वे इन कहानियों की हर पंक्ति से
गुजरे हैं, इसका क्रम लगाया है और संग्रह का नामकरण संस्कार भी उन्होंने ही
किया है। साथ ही उन पत्रिकाओं का भी आभारी हूँ जिनमें समय-समय पर ये छपती
रही हैं।
-मनु शर्मा
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book