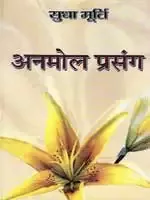|
व्यवहारिक मार्गदर्शिका >> अनमोल प्रसंग अनमोल प्रसंगसुधा मूर्ति
|
57 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत पुस्तक में अनमोल प्रसंगों का वर्णन किया गया है...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
इस पुस्तक में अपने व्यक्तिगत अनुभवों,अपनी यात्राओं तथा असामान्य
व्यक्तित्वों वाले सामान्य व्यक्तियों के साथ अपनी मुलाकातों का वर्णन
किया है। प्रस्तुत पुस्तक में वर्णित सभी प्रसंग लेखिका के जीवन के भोगे
हुए अनुभवों पर आधारित हैं। हमें पूर्ण विश्वास हैं, यह पुस्तक पाठकों को
सुखी, सफल एवं सार्थक जीवन जीने हेतु प्रेरणा प्रदान करेगी तथा उनके
व्यक्तित्व को निखारने एवं सँवारने में सहायक सिद्ध होगी।
भूमिका
हमारे यहाँ मनुष्य की योग्यता को सत्त्व, रजस
या तमस के
रूप में देखने की परंपरा है। यह एक तात्त्विक अवधारणा को अभिव्यक्त करने
का एक श्रेष्ठ भारतीय तरीका है, जो अन्य सभ्यताओं के लिए भी अपरिचित नहीं
है: ईश्वर की सभी रचनाओं में सिर्फ मानव को अच्छे या बुरे के बीच चयन करने
की योग्यता प्राप्त है और वह अपने चयन के अनुसार ही फल प्राप्त करता है।
कुछ सजग भाव से सात्त्विक कर्म की ओर उन्मुख होते हैं, कुछ जान-बूझकर तमस का जीवन पसंद करते हैं, कुछ तमस या रजस से शुरू करके स्वयं को सत्त्व की ओर ले जाते हैं। इन सब का कारण कर्म के विशाल ब्रह्मांडीय स्वरूप को समझा जा सकता है। जमशेतजी टाटा ने जीवन तथा कार्य के सिर्फ सात्त्विक दृष्टिकोण को अपनाया। उन्होंने उस समय अपने देश में औद्योगिक नींव रखी, शैक्षिक तथा शोध संस्थान शुरू किए और चैरिटी का नेटवर्क स्थापित किया, जब ऐसे विचार प्रचलित नहीं थे। दूसरी ओर, अल्फ्रेड नोबल ने अपनी प्रतिभा को डायनामाइट, गंधहीन गन पाउडर तथा गिलिग्नाइट बनाने में इस्तेमाल किया, जो जन-विनाश के कारक बने। फिर, शायद अपने जीवन की उपलब्धियों के परिणामों से दुःखी होकर उन्होंने अपनी सफलता का सात्त्विक इस्तेमाल करते हुए श्रेष्ठ कार्यों की पहचान के रूप में नोबल पुरस्कारों की स्थापना की।
सुधा मूर्ति ने अपनी चमक को घरेलू महिला के घेरे में नहीं छिपने दिया। वह अपनी नसों में शिक्षक के खून के साथ जनमी थीं और शिक्षण ऐसा व्यवसाय था जिसने विश्व को आकार देने में मदद की। परन्तु वह शिक्षकों की भीड़ में सिर्फ एक और चेहरा बनकर भी नहीं रहीं। अदृश्य परन्तु स्पष्ट रूप से महसूस होनेवाली शक्तियों ने उन्हें एक अपरिचित क्षेत्र की ओर उन्मुख किया। उन्होंने एक समाजवादी व्यक्ति से विवाह किया। जब पूँजीवाद के लाभ उनके सामने आए तो शिक्षक तथा समाजवादी की सहज वृत्तियाँ एक साथ मिलकर उन्हें जन-कल्याण के लिए जन-सेवा के क्षेत्र में ले गईं। एक शिक्षिका, पत्नी, माँ और एक सामान्य महिला रहते हुए सुधा मूर्ति एक संस्थान बन गई।
उन्होंने कोई भव्य इमारत नहीं बनाई। उनके कार्य में कोई सार्वजनिक घोषणाएँ शामिल नहीं हैं। कोई प्रतिमा, तख्ती या मेहराबदार रास्ते उनकी उपस्थिति को बयान नहीं करते। वह जनजातीय वनों, गरीबी से पीड़ित गाँवों और बीमारियों से तबाह समुदायों में जाती है। वह स्वयं ही मदद के योग्य समुदायों को पहचानती हैं। वह उनकी आवश्यकताओं के अनुसार मदद उपलब्ध कराती हैं। कुंठाएँ, अवरोध तथा लाल फीताशाही उनके कदमों को धीमा नहीं करते। यहाँ तक कि मानवीय लालसाएँ, जिनका वह अपने कार्य के दौरान काफी सामना करती हैं, उन्हें रोक नहीं पातीं। उनका कार्य उनका मिशन है। वह एक कर्मयोगी की तरह अपना कर्म करती हैं।
यह पुस्तक उनके कार्य तथा उसके प्रति उनकी प्रवृत्ति-दोनों का जीवंत वर्णन करती है। कन्नड़ की एक दक्ष कहानीकार सुधा ने ‘द न्यू संडे एक्सप्रेस’ में एक पाक्षिक स्तंभ का आरंभ करते हुए पहली बार अँग्रेजी में लिखा। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों, अपनी यात्राओं तथा असामान्य व्यक्तियोंवाले सामान्य व्यक्तियों के साथ अपनी मुलाकातों का वर्णन किया। अपनी ताजगी तथा स्पष्टता के कारण इस स्तंभ को काफी लोकप्रियता मिली। स्पष्टतः वह अपनी कलम से नहीं, अपने दिल से लिख रही थीं। आरंभ से ही यह स्पष्ट था कि मानव-प्रकृति में इन किस्सेनुमा अंतर्दृष्टियों को एक अधिक स्थायी रूप में व्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है, जो पत्रकारिता उपलब्ध नहीं करा सकती थी। इस पुस्तक के प्रकाशन द्वारा यह उद्देश्य पूरा हो गया।
हालाँकि यह बहुत खेद की बात होगी, यदि इन कहानियों का लाभ मात्र उन्हें पढ़ने के आनंद के साथ ही समाप्त हो जाए। यदि सुधा मूर्ति एक संदेश नहीं तो कुछ नहीं हैं। इंफोसिस की सफलता को दीन-हीन लोगों की सेवा करने के एक अवसर के रूप में बदलते हुए उन्होंने अन्य संपन्न लोगों तक एक संदेश पहुँचाया है। विकसित देशों में एक ओर सामाजिक सुधार कार्यक्रमों का कॉरपोरेट समर्थन और दूसरी ओर बौद्धिक रचनात्मकता सामान्य बात है; परन्तु यह हमारे देश में बहुत कम है। पश्चिम में संपन्न परिवारों के साथ जुड़े हुए फाउंडेशन जैसे फॉर्ड, रॉकफेलर तथा नफील्ड की बराबरी का भारत में कुछ नहीं है। उनमें से सबसे अधिक प्रतिष्ठित मैकआर्थर फाउंडेशन प्रतिभा पुरस्कार देती है। इसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि उसे किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं दिया गया। फिर भी वह चुपचाप महान् प्रतिभावाले लोगों-जैसे ए.के.रामानुजन-को पहचानकर उन्हें उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए फंड प्रदान करती है। इस प्रकार श्रेष्ठता, जो किसी देश के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण होती है, को समाज द्वारा विकसित किया जाता है। सुधा मूर्ति का कार्य तभी पूर्ण होगा जब अभावग्रस्त लोगों की मदद, मौलिकता की पहचान, बौद्धिक अन्वेषण को सुविधा प्रदान करने तथा सामान्यतः महानता को प्रेरित करने के लिए भारत में विशाल फाउंडेशनों की परंपरा आरंभ होगी।
कुछ सजग भाव से सात्त्विक कर्म की ओर उन्मुख होते हैं, कुछ जान-बूझकर तमस का जीवन पसंद करते हैं, कुछ तमस या रजस से शुरू करके स्वयं को सत्त्व की ओर ले जाते हैं। इन सब का कारण कर्म के विशाल ब्रह्मांडीय स्वरूप को समझा जा सकता है। जमशेतजी टाटा ने जीवन तथा कार्य के सिर्फ सात्त्विक दृष्टिकोण को अपनाया। उन्होंने उस समय अपने देश में औद्योगिक नींव रखी, शैक्षिक तथा शोध संस्थान शुरू किए और चैरिटी का नेटवर्क स्थापित किया, जब ऐसे विचार प्रचलित नहीं थे। दूसरी ओर, अल्फ्रेड नोबल ने अपनी प्रतिभा को डायनामाइट, गंधहीन गन पाउडर तथा गिलिग्नाइट बनाने में इस्तेमाल किया, जो जन-विनाश के कारक बने। फिर, शायद अपने जीवन की उपलब्धियों के परिणामों से दुःखी होकर उन्होंने अपनी सफलता का सात्त्विक इस्तेमाल करते हुए श्रेष्ठ कार्यों की पहचान के रूप में नोबल पुरस्कारों की स्थापना की।
सुधा मूर्ति ने अपनी चमक को घरेलू महिला के घेरे में नहीं छिपने दिया। वह अपनी नसों में शिक्षक के खून के साथ जनमी थीं और शिक्षण ऐसा व्यवसाय था जिसने विश्व को आकार देने में मदद की। परन्तु वह शिक्षकों की भीड़ में सिर्फ एक और चेहरा बनकर भी नहीं रहीं। अदृश्य परन्तु स्पष्ट रूप से महसूस होनेवाली शक्तियों ने उन्हें एक अपरिचित क्षेत्र की ओर उन्मुख किया। उन्होंने एक समाजवादी व्यक्ति से विवाह किया। जब पूँजीवाद के लाभ उनके सामने आए तो शिक्षक तथा समाजवादी की सहज वृत्तियाँ एक साथ मिलकर उन्हें जन-कल्याण के लिए जन-सेवा के क्षेत्र में ले गईं। एक शिक्षिका, पत्नी, माँ और एक सामान्य महिला रहते हुए सुधा मूर्ति एक संस्थान बन गई।
उन्होंने कोई भव्य इमारत नहीं बनाई। उनके कार्य में कोई सार्वजनिक घोषणाएँ शामिल नहीं हैं। कोई प्रतिमा, तख्ती या मेहराबदार रास्ते उनकी उपस्थिति को बयान नहीं करते। वह जनजातीय वनों, गरीबी से पीड़ित गाँवों और बीमारियों से तबाह समुदायों में जाती है। वह स्वयं ही मदद के योग्य समुदायों को पहचानती हैं। वह उनकी आवश्यकताओं के अनुसार मदद उपलब्ध कराती हैं। कुंठाएँ, अवरोध तथा लाल फीताशाही उनके कदमों को धीमा नहीं करते। यहाँ तक कि मानवीय लालसाएँ, जिनका वह अपने कार्य के दौरान काफी सामना करती हैं, उन्हें रोक नहीं पातीं। उनका कार्य उनका मिशन है। वह एक कर्मयोगी की तरह अपना कर्म करती हैं।
यह पुस्तक उनके कार्य तथा उसके प्रति उनकी प्रवृत्ति-दोनों का जीवंत वर्णन करती है। कन्नड़ की एक दक्ष कहानीकार सुधा ने ‘द न्यू संडे एक्सप्रेस’ में एक पाक्षिक स्तंभ का आरंभ करते हुए पहली बार अँग्रेजी में लिखा। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों, अपनी यात्राओं तथा असामान्य व्यक्तियोंवाले सामान्य व्यक्तियों के साथ अपनी मुलाकातों का वर्णन किया। अपनी ताजगी तथा स्पष्टता के कारण इस स्तंभ को काफी लोकप्रियता मिली। स्पष्टतः वह अपनी कलम से नहीं, अपने दिल से लिख रही थीं। आरंभ से ही यह स्पष्ट था कि मानव-प्रकृति में इन किस्सेनुमा अंतर्दृष्टियों को एक अधिक स्थायी रूप में व्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है, जो पत्रकारिता उपलब्ध नहीं करा सकती थी। इस पुस्तक के प्रकाशन द्वारा यह उद्देश्य पूरा हो गया।
हालाँकि यह बहुत खेद की बात होगी, यदि इन कहानियों का लाभ मात्र उन्हें पढ़ने के आनंद के साथ ही समाप्त हो जाए। यदि सुधा मूर्ति एक संदेश नहीं तो कुछ नहीं हैं। इंफोसिस की सफलता को दीन-हीन लोगों की सेवा करने के एक अवसर के रूप में बदलते हुए उन्होंने अन्य संपन्न लोगों तक एक संदेश पहुँचाया है। विकसित देशों में एक ओर सामाजिक सुधार कार्यक्रमों का कॉरपोरेट समर्थन और दूसरी ओर बौद्धिक रचनात्मकता सामान्य बात है; परन्तु यह हमारे देश में बहुत कम है। पश्चिम में संपन्न परिवारों के साथ जुड़े हुए फाउंडेशन जैसे फॉर्ड, रॉकफेलर तथा नफील्ड की बराबरी का भारत में कुछ नहीं है। उनमें से सबसे अधिक प्रतिष्ठित मैकआर्थर फाउंडेशन प्रतिभा पुरस्कार देती है। इसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि उसे किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं दिया गया। फिर भी वह चुपचाप महान् प्रतिभावाले लोगों-जैसे ए.के.रामानुजन-को पहचानकर उन्हें उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए फंड प्रदान करती है। इस प्रकार श्रेष्ठता, जो किसी देश के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण होती है, को समाज द्वारा विकसित किया जाता है। सुधा मूर्ति का कार्य तभी पूर्ण होगा जब अभावग्रस्त लोगों की मदद, मौलिकता की पहचान, बौद्धिक अन्वेषण को सुविधा प्रदान करने तथा सामान्यतः महानता को प्रेरित करने के लिए भारत में विशाल फाउंडेशनों की परंपरा आरंभ होगी।
टी.जे.एस.जॉर्ज, संपादकीय सलाहकार
लेखकीय
जब तक मैंने अपने कार्य के लिए ग्रामीण भारत
का अवलोकन,
उसकी खोज-बीन नहीं की थी, मैं अपने देश को नहीं समझ और जान पाई थी। मैंने
कई राज्यों की विस्तृत यात्रा की है और हजार से अधिक गाँवों में जाने का
अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। वहाँ मैंने तमाम व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव
बटोरे, जो मनुष्य जीवन को सुखद, सार्थक बनाने में महती भूमिका अदा करते
हैं। मानव-मस्तिष्क बहुत जटिल है। कुछ लोगों को धन और प्रसिद्धि की बहुत
आकांक्षा होती है, जबकि कुछ लोग शिक्षित न होने के बावजूद परिपक्व होते
हैं।
इस पुस्तक में वर्णित सभी प्रसंग जीवन के भोगे हुए अनुभवों पर आधारित हैं। प्रसंगों में वर्णित व्यक्तियों के मैंने सिर्फ नाम बदल दिए हैं और साथ ही कुछ अन्य वृत्तांत जोड़ दिए हैं। कभी-कभी साधारण लोगों, जिन्हें आगे बढ़ने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वे मेरे ‘गुरु’ हैं।
मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मेरी अंग्रेजी पुस्तक ‘वाइस एंड अदरवाइस’ का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो रहा है। यह पुस्तक अब तक भारत की दस भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। इसके सभी अध्याय मेरे जीवन में घटित वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं। सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा ही कद्र होती है, ऐसा मेरा मानना है।
मैं ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ के संपादकीय सलाहकार श्री टी.जे.एस जॉर्ज का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे समाचार-पत्र के लिए स्तंभ लिखने का आत्मविश्वास प्रदान किया। उन्होंने इस पुस्तक की भूमिका लिखी है। मैं ‘द वीक’ के श्री गोपालकृष्णन, ‘द हिंदुस्तान टाइम्स’ के श्री वीर सांघवी और ‘द हिंदू’ की सुश्री निर्मला लक्ष्मण को उनके समाचार-पत्र/पत्रिकाओं में प्रकाशित मेरे लेखों को पुनः प्रकाशित करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ ही मैं इस पुस्तक के अनुवाद के लिए सुश्री ज्योति की हृदय से आभारी हूँ।
अंत में, आप पाठकगण मेरे लिए बहुत महत्त्व रखते हैं। आप मेरी प्रेरणा हैं। आपके बिना एक लेखिका के रूप में मेरा कोई अस्तित्व नहीं होगा।
इस पुस्तक में वर्णित सभी प्रसंग जीवन के भोगे हुए अनुभवों पर आधारित हैं। प्रसंगों में वर्णित व्यक्तियों के मैंने सिर्फ नाम बदल दिए हैं और साथ ही कुछ अन्य वृत्तांत जोड़ दिए हैं। कभी-कभी साधारण लोगों, जिन्हें आगे बढ़ने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वे मेरे ‘गुरु’ हैं।
मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मेरी अंग्रेजी पुस्तक ‘वाइस एंड अदरवाइस’ का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो रहा है। यह पुस्तक अब तक भारत की दस भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। इसके सभी अध्याय मेरे जीवन में घटित वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं। सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा ही कद्र होती है, ऐसा मेरा मानना है।
मैं ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ के संपादकीय सलाहकार श्री टी.जे.एस जॉर्ज का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे समाचार-पत्र के लिए स्तंभ लिखने का आत्मविश्वास प्रदान किया। उन्होंने इस पुस्तक की भूमिका लिखी है। मैं ‘द वीक’ के श्री गोपालकृष्णन, ‘द हिंदुस्तान टाइम्स’ के श्री वीर सांघवी और ‘द हिंदू’ की सुश्री निर्मला लक्ष्मण को उनके समाचार-पत्र/पत्रिकाओं में प्रकाशित मेरे लेखों को पुनः प्रकाशित करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ ही मैं इस पुस्तक के अनुवाद के लिए सुश्री ज्योति की हृदय से आभारी हूँ।
अंत में, आप पाठकगण मेरे लिए बहुत महत्त्व रखते हैं। आप मेरी प्रेरणा हैं। आपके बिना एक लेखिका के रूप में मेरा कोई अस्तित्व नहीं होगा।
सुधा मूर्ति
१
ईमानदारी का संबंध संस्कार से है
तीन वर्ष पूर्व, जून की एक सुबह। मैं हर दिन
की तरह कन्नड़
अखबार पढ़ रही थी। उस दिन अखबार में एस.एस.एल.सी. का परीक्षा-परिणाम छपा
था। उत्तीर्ण छात्रों के अनुक्रमांक अंदर के पृष्ठों में छपे थे, वहीं
विशेष योग्यतावाले छात्रों के नाम व चित्रों से मुखपृष्ठ भरा पड़ा था।
अधिक अंक पानेवाले छात्रों के प्रति मेरा अधिक लगाव है। विशेष स्थान हासिल करना उनकी बुद्धिमानी ही नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य की पूर्ति-हेतु उनके परिश्रम व लगन को भी दर्शाता है। मेरा अपना अतीत, मेरा लालन-पालन एक प्रोफेसर परिवार में हुआ है। अध्यापकीय जीवन का मेरा अनुभव मेरी इस धारणा का जनक है।
प्रातःकालीन समाचार-पत्र में छपे इन चित्रों में मेरा ध्यान एक लड़के के चित्र पर अटका। मैं बरबस उसे निहारने लगी। अत्यधिक दुर्बल और पीला पड़ा चेहरा, किंतु उसकी आँखों में अद्भुत चमक थी। मुझे उसके विषय में और अधिक जानने की इच्छा हुई। तसवीर देखने के बाद जिज्ञासावश मैंने उसका नाम पढ़ा। उसका नाम ‘हनुमनथप्पा’ था, जिसे परीक्षा में आठवाँ स्थान प्राप्त हुआ था। केवल इतना ही उसके विषय में पता चल सका।
दूसरे दिन उसका फोटो उसके साक्षात्कार के साथ प्रकाशित हुआ, जिससे उसके बारे में और जानने की मेरी लालसा लगभग बढ़ गई। पता चला कि वह एक कुली का लड़का है। उसने एक सवाल के जवाब में स्वीकार किया था कि वह आगे पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ है, क्योंकि वह गाँव में रहता है और उसके पिता की दैनिक आय केवल चालीस रुपए है। हनुमनथप्पा अपने पिता की पाँच संतानों में सबसे बड़ा है और एकमात्र पिता ही परिवार का भरण-पोषण करनेवाला है। वह एक अनुसूचित जनजाति परिवार का सदस्य हैं।
यह जानकर इस होनहार बच्चे के लिए मुझे क्षोभ हुआ। हममें से अधिकतर लोग अपने बच्चों की अतिरिक्त पढ़ाई के लिए शिक्षक रखते हैं, अनेक ग्रंथ एवं मार्गदर्शक पुस्तकें खरीदने के अलावा अन्य सुविधाएँ भी प्रदान करने की कोशिश करते हैं, किंतु रामपुरा के हनुमनथप्पा की स्थिति भिन्न थी। सुविधाओं के अभाव में भी वह अच्छे अंक प्राप्त कर सका। अखबार पढ़ते-पढ़ते मैं उसके विषय में सोच ही रही थी कि मेरी नजर अपने पड़ोसी के आँगन के खड़े आम के पेड़ पर चली गई। मैंने उसे गौर से देखा, वह अपनी काली छाल, हरे पत्तों पर पड़ी ओस की बूँदों की चमक के साथ भविष्य में पूरे पके फल देनेवाला है। साथ ही पेड़ के पास गमले में एक पौधा था, जो आज भी उसी स्थिति में था, जैसा उसे रोपा गया था।
वह सुबह बड़ी शांत थी। हवा बहुत ठंडी व ताजा थी। मैं विचारों में डूबी हुई थी। घर के अंदर प्रेशर कुकर की सीटी ने जब सन्नाटे को तोड़ा तो पता चला कि मैं काफी देर से यहाँ पर बैठी हूँ।
साक्षात्कार में हनुमनथप्पा का पूरा पता छपा था। बिना समय गँवाए मैंने तुरन्त उसके पते पर एक पोस्टकार्ड में दो पंक्तियाँ लिख दीं कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ, अतः जानना चाहा कि क्या वह बंगलौर आ सकता है ? तभी मेरे पिता प्रातःकालीन भ्रमण से वापस आ गए। उन्होंने मेरा पत्र पढ़ा और कहा, ‘उसके पास इतनी दूर आने के लिए पैसे कहाँ से आएँगे ! अगर तुम उसे बुलाना चाहती हो तो बस का किराया तथा कुछ और पैसे भेज दो, जिससे वह अपने लिए नए कपड़े खरीद सके।’ तब मैंने उस पत्र में तीसरी पंक्ति जोड़ दी कि ‘तुम्हारे आने-जाने व कपड़ों की खरीद पर हुए व्यय का भुगतान किया जाएगा।’ चार दिनों के अंदर मुझे एक पोस्टकार्ड मिला, जिसपर दो पंक्तियाँ लिखी थीं-पहली, ‘मैं पत्र के लिए धन्यवाद देता हूँ,’ व दूसरी,‘बंगलौर आकर आपसे मिलने की मेरी इच्छा है।’
तुरन्त मैंने अपने कार्यालय का पूरा पता और कुछ पैसे उसके लिए भेज दिए। अंततः जब वह मेरे कार्यालय में पहुँचा तो मुझे वह भयभीत, भटके हुए बछड़े की तरह लगा। शायद बंगलौर आने का उसका पहला मौका था। वह विनयशील था। साफ-सुथरे कपड़े पहने हुए था। बालों में कंघी की हुई थी। उसकी आँखों में चमक अब भी विद्यमान थी।
मैंने मुख्य मुद्दे पर वार्ता करते हुए कहा, ‘हम तुम्हारी शैक्षिक योग्यता से प्रसन्न हैं। क्या आगे पढ़ना चाहोगे ? हम तुम्हें आगे पढ़ाएँगे-अर्थात् जिस विषय की शिक्षा जहाँ भी प्राप्त करना चाहो, उसके लिए पूरा व्यय वहन करेंगे।’
उसने कोई उत्तर नहीं दिया।
मेरे वरिष्ठ साथी, जो मेरे साथ ही थे, ने मुस्कराते हुए कहा, ‘जल्दबाजी मत करो। अपने प्रस्ताव पर शाम तक कुछ सोचने का समय दो इसे, तभी यह कुछ कह सकेगा।’
जब हनुमनथप्पा वापस जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने बहुत ही सधे हुए स्वर में धीमे से कहा, ‘मैडम, मैं शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,बेल्लारी में आगे की अपनी शिक्षा पाना चाहता हूँ। वह स्थान मेरे गाँव के निकट है।’
मैंने तुरन्त स्वीकृति दे दी, किन्तु उससे जानना चाहा कि क्या कोई अन्य कोर्स वह करना चाहेगा। मेरा उद्देश्य उसे यह समझाना था कि हम उसकी इच्छा के अनुसार कोर्स करने हेतु शुल्क देने के लिए तैयार हैं, परन्तु वह बालक अपने विचार पर दृढ़ था और जानता था कि उसे क्या चाहिए।
‘मैं कितनी राशि तुम्हें प्रत्येक महीने भेजूँ ? क्या महाविद्यालय में आवासीय व्यवस्था है? मैंने पूछा।
उसने कहा कि पता करने पर वह सूचित करेगा।
दो दिन बाद बहुत ही खूबसूरत लिखावट में उसका पत्र मिला, जिसमें उसने लिखा था कि उसे तीन सौ रुपए महीने की आवश्यकता पड़ेगी। वह अपने मित्र के साथ किराए के एक कमरे में रहेगा। दोनों स्वयं अपना भोजन तैयार करेंगे, जिससे खर्च कम होगा। मैंने उसे छह महीने के लिए एक हजार आठ सौ रुपए तुरन्त भेज दिए, जिसकी प्राप्ति-सूचना के साथ उसने कृतज्ञता व्यक्त की।
समय बीता। एक दिन मुझे अचानक याद आया कि हनुमनथप्पा के लिए अगले छह महीने की खर्च-राशि भेजनी है। अतः पुनः एक हजार आठ सौ रुपए का बैंक ड्राफ्ट भेज दिया।
धनराशि की प्राप्ति की सूचना के साथ कुछ रुपए भी लिफाफे में मिलने से मुझे आश्चर्य हुआ। उसने पत्र में लिखा था-‘मैडम, आपकी बड़ी कृपा है कि अगले छह महीने के लिए अग्रिम राशि आपने भेजी, किंतु मैं पिछले दो महीने से बेल्लारी में नहीं था। एक महीने कॉलेज की छुट्टी थी और एक महीने हड़ताल चलती रही, अतः मैं अपने घर पर ही रहा। उन महीनों में मेरा खर्च तीन सौ रुपए से कम रहा। अतः बचत के तीन सौ रुपए वापस भेज रहा हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें।’
मैं चकित रह गई-इतनी गरीबी होने पर भी इस तरह की ईमानदारी !
हनुमनथप्पा को मालूम था कि महीने के खर्च के रूप में भेजी गई राशि में से कुछ भी वापस मिलने की आशा मुझे नहीं थी, फिर भी उसने उस राशि को वापस किया। वह अविश्वसनीय, किन्तु सत्य घटना है।
अनुभव ने मुझे सिखाया कि ईमानदारी किसी विशेष वर्ग, शिक्षा या पूँजी की देन नहीं है। इसकी शिक्षा किसी विश्वविद्यालय में भी नहीं ली जा सकती। अधिकतर लोगों में यह गुण स्वाभाविक होता है- संस्कारजनित। मुझे नहीं सूझा कि एक ग्रामीण बालक की ईमानदारी पर क्या प्रतिक्रिया जताऊँ। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह हनुमनथप्पा व उसके परिवार पर दयादृष्टि रखे।
अधिक अंक पानेवाले छात्रों के प्रति मेरा अधिक लगाव है। विशेष स्थान हासिल करना उनकी बुद्धिमानी ही नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य की पूर्ति-हेतु उनके परिश्रम व लगन को भी दर्शाता है। मेरा अपना अतीत, मेरा लालन-पालन एक प्रोफेसर परिवार में हुआ है। अध्यापकीय जीवन का मेरा अनुभव मेरी इस धारणा का जनक है।
प्रातःकालीन समाचार-पत्र में छपे इन चित्रों में मेरा ध्यान एक लड़के के चित्र पर अटका। मैं बरबस उसे निहारने लगी। अत्यधिक दुर्बल और पीला पड़ा चेहरा, किंतु उसकी आँखों में अद्भुत चमक थी। मुझे उसके विषय में और अधिक जानने की इच्छा हुई। तसवीर देखने के बाद जिज्ञासावश मैंने उसका नाम पढ़ा। उसका नाम ‘हनुमनथप्पा’ था, जिसे परीक्षा में आठवाँ स्थान प्राप्त हुआ था। केवल इतना ही उसके विषय में पता चल सका।
दूसरे दिन उसका फोटो उसके साक्षात्कार के साथ प्रकाशित हुआ, जिससे उसके बारे में और जानने की मेरी लालसा लगभग बढ़ गई। पता चला कि वह एक कुली का लड़का है। उसने एक सवाल के जवाब में स्वीकार किया था कि वह आगे पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ है, क्योंकि वह गाँव में रहता है और उसके पिता की दैनिक आय केवल चालीस रुपए है। हनुमनथप्पा अपने पिता की पाँच संतानों में सबसे बड़ा है और एकमात्र पिता ही परिवार का भरण-पोषण करनेवाला है। वह एक अनुसूचित जनजाति परिवार का सदस्य हैं।
यह जानकर इस होनहार बच्चे के लिए मुझे क्षोभ हुआ। हममें से अधिकतर लोग अपने बच्चों की अतिरिक्त पढ़ाई के लिए शिक्षक रखते हैं, अनेक ग्रंथ एवं मार्गदर्शक पुस्तकें खरीदने के अलावा अन्य सुविधाएँ भी प्रदान करने की कोशिश करते हैं, किंतु रामपुरा के हनुमनथप्पा की स्थिति भिन्न थी। सुविधाओं के अभाव में भी वह अच्छे अंक प्राप्त कर सका। अखबार पढ़ते-पढ़ते मैं उसके विषय में सोच ही रही थी कि मेरी नजर अपने पड़ोसी के आँगन के खड़े आम के पेड़ पर चली गई। मैंने उसे गौर से देखा, वह अपनी काली छाल, हरे पत्तों पर पड़ी ओस की बूँदों की चमक के साथ भविष्य में पूरे पके फल देनेवाला है। साथ ही पेड़ के पास गमले में एक पौधा था, जो आज भी उसी स्थिति में था, जैसा उसे रोपा गया था।
वह सुबह बड़ी शांत थी। हवा बहुत ठंडी व ताजा थी। मैं विचारों में डूबी हुई थी। घर के अंदर प्रेशर कुकर की सीटी ने जब सन्नाटे को तोड़ा तो पता चला कि मैं काफी देर से यहाँ पर बैठी हूँ।
साक्षात्कार में हनुमनथप्पा का पूरा पता छपा था। बिना समय गँवाए मैंने तुरन्त उसके पते पर एक पोस्टकार्ड में दो पंक्तियाँ लिख दीं कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ, अतः जानना चाहा कि क्या वह बंगलौर आ सकता है ? तभी मेरे पिता प्रातःकालीन भ्रमण से वापस आ गए। उन्होंने मेरा पत्र पढ़ा और कहा, ‘उसके पास इतनी दूर आने के लिए पैसे कहाँ से आएँगे ! अगर तुम उसे बुलाना चाहती हो तो बस का किराया तथा कुछ और पैसे भेज दो, जिससे वह अपने लिए नए कपड़े खरीद सके।’ तब मैंने उस पत्र में तीसरी पंक्ति जोड़ दी कि ‘तुम्हारे आने-जाने व कपड़ों की खरीद पर हुए व्यय का भुगतान किया जाएगा।’ चार दिनों के अंदर मुझे एक पोस्टकार्ड मिला, जिसपर दो पंक्तियाँ लिखी थीं-पहली, ‘मैं पत्र के लिए धन्यवाद देता हूँ,’ व दूसरी,‘बंगलौर आकर आपसे मिलने की मेरी इच्छा है।’
तुरन्त मैंने अपने कार्यालय का पूरा पता और कुछ पैसे उसके लिए भेज दिए। अंततः जब वह मेरे कार्यालय में पहुँचा तो मुझे वह भयभीत, भटके हुए बछड़े की तरह लगा। शायद बंगलौर आने का उसका पहला मौका था। वह विनयशील था। साफ-सुथरे कपड़े पहने हुए था। बालों में कंघी की हुई थी। उसकी आँखों में चमक अब भी विद्यमान थी।
मैंने मुख्य मुद्दे पर वार्ता करते हुए कहा, ‘हम तुम्हारी शैक्षिक योग्यता से प्रसन्न हैं। क्या आगे पढ़ना चाहोगे ? हम तुम्हें आगे पढ़ाएँगे-अर्थात् जिस विषय की शिक्षा जहाँ भी प्राप्त करना चाहो, उसके लिए पूरा व्यय वहन करेंगे।’
उसने कोई उत्तर नहीं दिया।
मेरे वरिष्ठ साथी, जो मेरे साथ ही थे, ने मुस्कराते हुए कहा, ‘जल्दबाजी मत करो। अपने प्रस्ताव पर शाम तक कुछ सोचने का समय दो इसे, तभी यह कुछ कह सकेगा।’
जब हनुमनथप्पा वापस जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने बहुत ही सधे हुए स्वर में धीमे से कहा, ‘मैडम, मैं शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,बेल्लारी में आगे की अपनी शिक्षा पाना चाहता हूँ। वह स्थान मेरे गाँव के निकट है।’
मैंने तुरन्त स्वीकृति दे दी, किन्तु उससे जानना चाहा कि क्या कोई अन्य कोर्स वह करना चाहेगा। मेरा उद्देश्य उसे यह समझाना था कि हम उसकी इच्छा के अनुसार कोर्स करने हेतु शुल्क देने के लिए तैयार हैं, परन्तु वह बालक अपने विचार पर दृढ़ था और जानता था कि उसे क्या चाहिए।
‘मैं कितनी राशि तुम्हें प्रत्येक महीने भेजूँ ? क्या महाविद्यालय में आवासीय व्यवस्था है? मैंने पूछा।
उसने कहा कि पता करने पर वह सूचित करेगा।
दो दिन बाद बहुत ही खूबसूरत लिखावट में उसका पत्र मिला, जिसमें उसने लिखा था कि उसे तीन सौ रुपए महीने की आवश्यकता पड़ेगी। वह अपने मित्र के साथ किराए के एक कमरे में रहेगा। दोनों स्वयं अपना भोजन तैयार करेंगे, जिससे खर्च कम होगा। मैंने उसे छह महीने के लिए एक हजार आठ सौ रुपए तुरन्त भेज दिए, जिसकी प्राप्ति-सूचना के साथ उसने कृतज्ञता व्यक्त की।
समय बीता। एक दिन मुझे अचानक याद आया कि हनुमनथप्पा के लिए अगले छह महीने की खर्च-राशि भेजनी है। अतः पुनः एक हजार आठ सौ रुपए का बैंक ड्राफ्ट भेज दिया।
धनराशि की प्राप्ति की सूचना के साथ कुछ रुपए भी लिफाफे में मिलने से मुझे आश्चर्य हुआ। उसने पत्र में लिखा था-‘मैडम, आपकी बड़ी कृपा है कि अगले छह महीने के लिए अग्रिम राशि आपने भेजी, किंतु मैं पिछले दो महीने से बेल्लारी में नहीं था। एक महीने कॉलेज की छुट्टी थी और एक महीने हड़ताल चलती रही, अतः मैं अपने घर पर ही रहा। उन महीनों में मेरा खर्च तीन सौ रुपए से कम रहा। अतः बचत के तीन सौ रुपए वापस भेज रहा हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें।’
मैं चकित रह गई-इतनी गरीबी होने पर भी इस तरह की ईमानदारी !
हनुमनथप्पा को मालूम था कि महीने के खर्च के रूप में भेजी गई राशि में से कुछ भी वापस मिलने की आशा मुझे नहीं थी, फिर भी उसने उस राशि को वापस किया। वह अविश्वसनीय, किन्तु सत्य घटना है।
अनुभव ने मुझे सिखाया कि ईमानदारी किसी विशेष वर्ग, शिक्षा या पूँजी की देन नहीं है। इसकी शिक्षा किसी विश्वविद्यालय में भी नहीं ली जा सकती। अधिकतर लोगों में यह गुण स्वाभाविक होता है- संस्कारजनित। मुझे नहीं सूझा कि एक ग्रामीण बालक की ईमानदारी पर क्या प्रतिक्रिया जताऊँ। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह हनुमनथप्पा व उसके परिवार पर दयादृष्टि रखे।
२
मानवीय दुर्बलता
कई वर्ष पूर्व मैं मुख्य प्रणाली विश्लेषक के
पद पर
कार्यरत थी। मुझे परियोजना-संबंधी कार्य के लिए अकसर इधर-उधर यात्रा करनी
पड़ती थी, कभी छोटे से गाँव में तो कभी निकटवर्ती शहर में। प्रायः अवकाश
के दिनों में भी मुझे यात्रा करनी पड़ती थी।
एक शुक्रवार की बात है, मैं लंबे सप्ताहांत की बात सोच रही थी, क्योंकि आगामी सोमवार को किसी पर्व की छुट्टी का दिन था, जिसका उपयोग हम बहनों ने अपने पैतृक स्थान शिगाँव में अपनी नानी के पास जाने का कार्यक्रम बनाया था।
मैं बेसब्री से शुक्रवार के बीतने का इंतजार कर रही थी। रविवार को पूर्णमासी की रात थी, अतः चाँदनी में रात्रि-भोजन का विशेष प्रबंध किया गया था। उत्तरी कर्नाटक के निवासियों के लिए चाँद की रोशनी में रात्रि-भोजन करना परिवार की रुचि के अनुसार होता था। हम सब दिन भर का काम समाप्त कर ही रहे थे कि मुझे किसी की आवाज सुनाई दी, ‘कुलकर्णी, क्या तुम मेरे दफ्तर आ सकती हो ?’ मेरा मन बुझ गया। यह मेरा उच्चाधिकारी था, जो मेरे विवाह-पूर्व के नाम से पुकार रहा था। उसके स्वर से पता चल रहा था कि कोई जरूरी काम है। मैं कार्यालय से बाहर निकलने ही वाली थी, मुझे रुकना पड़ा यह जानने के लिए कि आखिर उसे चाहिए क्या ?
‘आपके कार्य में विघ्न डालने के लिए मुझे खेद है, किंतु आपकी सेवाओं की तुरन्त आवश्यकता है।’ उसने एक पत्र मुझे थमाते हुए पढ़ने को दिया। उस पत्र में मुझे एक परियोजना-स्थल पर अगले दो दिन के अंदर पहुँचना था। ‘कोई बात नहीं, श्रीमान्, मैं चली जाऊँगी।’ मैंने कहा।
मुझे दिन भर व सप्ताह भर काम करने की आदत सी हो गई थी। अतः यात्रा का कार्यक्रम निरस्त करने का मुझे तनिक भी मलाल नहीं हुआ। मुझे बाहर घूमने जाने से अधिक सुख अपने काम में व्यस्त रहने पर मिलता है।
अगली सुबह मैं परियोजना-स्थल पर गई। जब मैं नगर में पहुँची तब दोपहर हो चुकी थी, किन्तु लगा, जैसे वहाँ दिन तभी शुरू हुआ हो। छोटा सा नगर। दुकानें अभी खुल रही थीं। लोग अपने-अपने काम के लिए बाहर निकले ही थे। बस से उतरकर जैसे ही मैं आगे बढ़ी, एक लड़का मेरे पास आकर बोला, ‘मैडम,मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे बस स्टॉप पर ही आपका स्वागत करना था।’ वह हमारे ग्राहक का प्रतिनिधि था, जो मुझे अपने कार्यालय तक ले जाने के लिए आया था। हम थोड़ा सा पैदल चलकर उसके कार्यालय में पहुँच गये थे। छोटा सा दफ्तर यद्यपि आधुनिक साज-सज्जाविहीन था, किंतु मरम्मत किए गए पुराने फर्नीचर को साफ करके रखा गया था। सबकुछ तरतीब से रखा हुआ था। वे लोग मेरी प्रतीक्षा में थे। जैसे ही मैं बैठी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो शीतल व ताजा छाछ मुझे पिलाई, उससे मुझे बहुत ताजगी महसूस हुई।
अपना कार्य शुरू करने से पूर्व मेरा परिचय एक साफ व चुस्त कपड़े पहने एक युवक से कराया गया, जो मेरे साथ काम में तालमेल के हेतु सहयोगी नियुक्त हुआ था। वह संस्कारयुक्त, आत्मविश्वासी एवं चतुर व्यक्ति लगा। मुझे व्यावसायिक अनुभव था। मुझे बताया गया कि वह शहर का सबसे अधिक पढ़ा-लिखा व जानकार व्यक्ति है। उसने अपने काम के संबंध में कुशलतापूर्वक अभिलेखों को तैयार कर रखा था, जिससे हमारा कार्य अपेक्षाकृत शीघ्र पूरा हो गया। वहाँ से आने के पूर्व मैं उसकी प्रशंसा करना नहीं भूली। मेरे द्वारा की गई प्रशंसा के शब्दों से वह झेंप सा गया। उसका रंग पीला सा पड़ गया। उसने जोर दिया कि मैं पास में ही उसके घर चाय पर अवश्य पहुँचूँ।
मैं उसके घर पर गई। उसका मकान सुंदर,करीने से सजा हुआ था। चाय आने तक उसके साथ बातचीत में व्यक्तिगत रुझान सा हो गया था। उसने अपने माता-पिता व अपने पहले काम के विषय में बताया। उसने अपनी पत्नी व दो वर्ष के बेटे से परिचय करवाया। अपनी पत्नी के स्वादिष्ट खाना बनाने और उसकी सुंदर आवाज की प्रशंसा तथा पढ़ाई के दौरान स्कूल में उसके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का वर्णन करते हुए वह पुलकित हो रहा था। तब उसने अपने बेटे के विषय में बताया, जो तभी आकार मेरी बगल में खड़ा हो गया था-चुपचाप हाथ जोड़े, मानो उसे इस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया गया हो। जैसे ही पिता ने उसे राइम (तुकांत कविता) सुनाने के लिए कहा, उसने तुरंत अपनी तोतली बोली में कविता-पाठ शुरू कर दिया।
मैंने उसके कविता-पाठ की प्रशंसा सिर हिलाकर की। उसके पिता को बच्चे के गुणों की इस प्रकार हलकी प्रशंसा से संतुष्टि नहीं हुई तो पिता ने बच्चे से दीवार पर टँगे कैलेंडर/चार्ट के सभी अक्षर पहचानने के लिए कहा। यह बच्चे के लिए सबसे अधिक कठिन काम होता है, फिर भी हर पिता इसके लिए बच्चे पर जोर देता है-बेचारे बच्चे।
यब सब करीब आधे घंटे तक चला, तब तक, जब तक बच्चे ने खीजना शुरू नहीं कर दिया। माँ चुपके से बच्चे को वहाँ से ले गई, शायद उसे फुसलाने और चॉकलेट खिलाने।
मुझे लगा कि पिता बच्चे की प्रशंसा में मुझसे कुछ सुनना चाहता था, तो मैं बोली, ‘अपनी आयु में यह बच्चा बहुत होशियार और होनहार है।’
उसने गर्व से कहा, ‘स्वाभाविक है, क्योंकि मैंने उसे बचपन से ही इस प्रकार सिखाया है।’
मुझे लगा कि वह उस दो वर्ष के बच्चे को जन्म से ही प्रशिक्षित कर रहा था।
मैंने पूछा, ‘आपके अनुसार केवल इस प्रकार की शिक्षा देकर बच्चा होशियार व चतुर बन सकता है,क्यों ?’
‘नहीं-नहीं, वंश-परंपरा एवं जैविक गुण भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। मेरा बच्चा मुझपर गया है।’
उस व्यक्ति का चेहरा गर्व से दमकने लगा तथा मैं और अधिक सुनने के लिए लालायित हो गई। आखिर मुझे बस के आने तक के एक घंटे का समय तो बिताना ही था।
‘आप अपने कॉलेज के दिनों में अच्छे विद्यार्थी रहे होंगे ?’ मैंने कुरेदा।
‘हाँ, मैं अच्छा विद्यार्थी था। मैं स्कूल व कॉलेज में प्रथम आता था।’ आत्मप्रशंसा में उसने कहा।
‘आपने स्नातक शिक्षा कहाँ पाई ?’ मैंने उत्सुकतापूर्वक पूछा।
‘मैंने बी.वी.बी.इंजीनियरिंग कॉलेज, हुबली से स्नातक उपाधि प्राप्त की।’
मैं चौकन्नी हुई। मैं हुबली से परिचित हूँ। उसे कॉलेज को भी मैं जानती हूँ।
‘किस साल ?’ मैंने पूछा।
‘वर्ष 1972 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था।’
‘क्या आपको स्वर्ण पदक मिला था ?’ मैंने जानना चाहा।
‘हाँ, मुझे उस वर्ष का स्वर्ण पदक मिला था।’ आत्मसंतुष्टि और गर्व के साथ उसने कहा।
तब से मैं उस व्यक्ति को समझने लगी थी। और जो मैंने देखा, उससे मुझे निराशा हुई।
‘क्या मैं आपका स्वर्ण पदक देख सकती हूँ ?’ मैंने पूछा।
सहसा कमरे का वातावरण बदल गया, ‘क्यों, क्या आपको मुझपर विश्वास नहीं है?’ उसका स्वर भर्रा गया।
‘नहीं। मैं वर्ष 1972 में प्राप्त आपका स्वर्ण पदक देखना चाहती हूँ।’ मैंने दोहराया।
‘वह मेरे लिए बहुत मूल्यवान् है, इसलिए मैंने उसे बैंक के लॉकर में रखा है।’ उसने कहा।
मैं भी छोड़नेवाली नहीं थी, ‘किस बैंक में ?’
‘मैं आपको यह सब विवरण क्यों दूँ ?’ मेरी बात से वह चिढ़ सा गया।
तब तक सब कुछ साफ हो गया था। शायद वह भी समझ गया था। सत्कार का समय निकल गया था। मेरी बस का समय हो गया था और मेरे वहाँ से जाने का भी।
द्वार की ओर बढ़ते हुए मैंने उससे कहा, ‘मुझे आपके स्वर्ण पदक व बैंक को जानने की कोई इच्छा नहीं है, यह मेरा काम नहीं है। किंतु मुझे विश्वास है कि वह स्वर्ण पदक आपके पास नहीं है।’
‘आप यह कैसे कह सकती हैं और वह भी इतने विश्वास के साथ?’ अब तक वह आगबबूला हो गया था।
‘क्योंकि सन् 1972 में स्वर्ण पदक मुझे मिला था।’ मैंने धीरे से उदासी भरे स्वर में कहा, ‘और प्रतिवर्ष केवल एक ही स्वर्ण पदक दिया जाता है।’
इसे जानकर वह भौंचक्का रह गया और मेरी ओर एकटक देखने लगा। मैंने उसकी ओर देखा और नम्रतापूर्वक कहा, ‘आप काफी होशियार हैं। अपने काम में प्रवीण हैं। फिर आपको झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है ? इससे आपको क्या मिलेगा ?’
सामने का द्वार मेरे पीछे भड़ाक से बंद हुआ। मुझे यही उत्तर मिलना था।
एक शुक्रवार की बात है, मैं लंबे सप्ताहांत की बात सोच रही थी, क्योंकि आगामी सोमवार को किसी पर्व की छुट्टी का दिन था, जिसका उपयोग हम बहनों ने अपने पैतृक स्थान शिगाँव में अपनी नानी के पास जाने का कार्यक्रम बनाया था।
मैं बेसब्री से शुक्रवार के बीतने का इंतजार कर रही थी। रविवार को पूर्णमासी की रात थी, अतः चाँदनी में रात्रि-भोजन का विशेष प्रबंध किया गया था। उत्तरी कर्नाटक के निवासियों के लिए चाँद की रोशनी में रात्रि-भोजन करना परिवार की रुचि के अनुसार होता था। हम सब दिन भर का काम समाप्त कर ही रहे थे कि मुझे किसी की आवाज सुनाई दी, ‘कुलकर्णी, क्या तुम मेरे दफ्तर आ सकती हो ?’ मेरा मन बुझ गया। यह मेरा उच्चाधिकारी था, जो मेरे विवाह-पूर्व के नाम से पुकार रहा था। उसके स्वर से पता चल रहा था कि कोई जरूरी काम है। मैं कार्यालय से बाहर निकलने ही वाली थी, मुझे रुकना पड़ा यह जानने के लिए कि आखिर उसे चाहिए क्या ?
‘आपके कार्य में विघ्न डालने के लिए मुझे खेद है, किंतु आपकी सेवाओं की तुरन्त आवश्यकता है।’ उसने एक पत्र मुझे थमाते हुए पढ़ने को दिया। उस पत्र में मुझे एक परियोजना-स्थल पर अगले दो दिन के अंदर पहुँचना था। ‘कोई बात नहीं, श्रीमान्, मैं चली जाऊँगी।’ मैंने कहा।
मुझे दिन भर व सप्ताह भर काम करने की आदत सी हो गई थी। अतः यात्रा का कार्यक्रम निरस्त करने का मुझे तनिक भी मलाल नहीं हुआ। मुझे बाहर घूमने जाने से अधिक सुख अपने काम में व्यस्त रहने पर मिलता है।
अगली सुबह मैं परियोजना-स्थल पर गई। जब मैं नगर में पहुँची तब दोपहर हो चुकी थी, किन्तु लगा, जैसे वहाँ दिन तभी शुरू हुआ हो। छोटा सा नगर। दुकानें अभी खुल रही थीं। लोग अपने-अपने काम के लिए बाहर निकले ही थे। बस से उतरकर जैसे ही मैं आगे बढ़ी, एक लड़का मेरे पास आकर बोला, ‘मैडम,मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे बस स्टॉप पर ही आपका स्वागत करना था।’ वह हमारे ग्राहक का प्रतिनिधि था, जो मुझे अपने कार्यालय तक ले जाने के लिए आया था। हम थोड़ा सा पैदल चलकर उसके कार्यालय में पहुँच गये थे। छोटा सा दफ्तर यद्यपि आधुनिक साज-सज्जाविहीन था, किंतु मरम्मत किए गए पुराने फर्नीचर को साफ करके रखा गया था। सबकुछ तरतीब से रखा हुआ था। वे लोग मेरी प्रतीक्षा में थे। जैसे ही मैं बैठी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो शीतल व ताजा छाछ मुझे पिलाई, उससे मुझे बहुत ताजगी महसूस हुई।
अपना कार्य शुरू करने से पूर्व मेरा परिचय एक साफ व चुस्त कपड़े पहने एक युवक से कराया गया, जो मेरे साथ काम में तालमेल के हेतु सहयोगी नियुक्त हुआ था। वह संस्कारयुक्त, आत्मविश्वासी एवं चतुर व्यक्ति लगा। मुझे व्यावसायिक अनुभव था। मुझे बताया गया कि वह शहर का सबसे अधिक पढ़ा-लिखा व जानकार व्यक्ति है। उसने अपने काम के संबंध में कुशलतापूर्वक अभिलेखों को तैयार कर रखा था, जिससे हमारा कार्य अपेक्षाकृत शीघ्र पूरा हो गया। वहाँ से आने के पूर्व मैं उसकी प्रशंसा करना नहीं भूली। मेरे द्वारा की गई प्रशंसा के शब्दों से वह झेंप सा गया। उसका रंग पीला सा पड़ गया। उसने जोर दिया कि मैं पास में ही उसके घर चाय पर अवश्य पहुँचूँ।
मैं उसके घर पर गई। उसका मकान सुंदर,करीने से सजा हुआ था। चाय आने तक उसके साथ बातचीत में व्यक्तिगत रुझान सा हो गया था। उसने अपने माता-पिता व अपने पहले काम के विषय में बताया। उसने अपनी पत्नी व दो वर्ष के बेटे से परिचय करवाया। अपनी पत्नी के स्वादिष्ट खाना बनाने और उसकी सुंदर आवाज की प्रशंसा तथा पढ़ाई के दौरान स्कूल में उसके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का वर्णन करते हुए वह पुलकित हो रहा था। तब उसने अपने बेटे के विषय में बताया, जो तभी आकार मेरी बगल में खड़ा हो गया था-चुपचाप हाथ जोड़े, मानो उसे इस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया गया हो। जैसे ही पिता ने उसे राइम (तुकांत कविता) सुनाने के लिए कहा, उसने तुरंत अपनी तोतली बोली में कविता-पाठ शुरू कर दिया।
मैंने उसके कविता-पाठ की प्रशंसा सिर हिलाकर की। उसके पिता को बच्चे के गुणों की इस प्रकार हलकी प्रशंसा से संतुष्टि नहीं हुई तो पिता ने बच्चे से दीवार पर टँगे कैलेंडर/चार्ट के सभी अक्षर पहचानने के लिए कहा। यह बच्चे के लिए सबसे अधिक कठिन काम होता है, फिर भी हर पिता इसके लिए बच्चे पर जोर देता है-बेचारे बच्चे।
यब सब करीब आधे घंटे तक चला, तब तक, जब तक बच्चे ने खीजना शुरू नहीं कर दिया। माँ चुपके से बच्चे को वहाँ से ले गई, शायद उसे फुसलाने और चॉकलेट खिलाने।
मुझे लगा कि पिता बच्चे की प्रशंसा में मुझसे कुछ सुनना चाहता था, तो मैं बोली, ‘अपनी आयु में यह बच्चा बहुत होशियार और होनहार है।’
उसने गर्व से कहा, ‘स्वाभाविक है, क्योंकि मैंने उसे बचपन से ही इस प्रकार सिखाया है।’
मुझे लगा कि वह उस दो वर्ष के बच्चे को जन्म से ही प्रशिक्षित कर रहा था।
मैंने पूछा, ‘आपके अनुसार केवल इस प्रकार की शिक्षा देकर बच्चा होशियार व चतुर बन सकता है,क्यों ?’
‘नहीं-नहीं, वंश-परंपरा एवं जैविक गुण भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। मेरा बच्चा मुझपर गया है।’
उस व्यक्ति का चेहरा गर्व से दमकने लगा तथा मैं और अधिक सुनने के लिए लालायित हो गई। आखिर मुझे बस के आने तक के एक घंटे का समय तो बिताना ही था।
‘आप अपने कॉलेज के दिनों में अच्छे विद्यार्थी रहे होंगे ?’ मैंने कुरेदा।
‘हाँ, मैं अच्छा विद्यार्थी था। मैं स्कूल व कॉलेज में प्रथम आता था।’ आत्मप्रशंसा में उसने कहा।
‘आपने स्नातक शिक्षा कहाँ पाई ?’ मैंने उत्सुकतापूर्वक पूछा।
‘मैंने बी.वी.बी.इंजीनियरिंग कॉलेज, हुबली से स्नातक उपाधि प्राप्त की।’
मैं चौकन्नी हुई। मैं हुबली से परिचित हूँ। उसे कॉलेज को भी मैं जानती हूँ।
‘किस साल ?’ मैंने पूछा।
‘वर्ष 1972 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था।’
‘क्या आपको स्वर्ण पदक मिला था ?’ मैंने जानना चाहा।
‘हाँ, मुझे उस वर्ष का स्वर्ण पदक मिला था।’ आत्मसंतुष्टि और गर्व के साथ उसने कहा।
तब से मैं उस व्यक्ति को समझने लगी थी। और जो मैंने देखा, उससे मुझे निराशा हुई।
‘क्या मैं आपका स्वर्ण पदक देख सकती हूँ ?’ मैंने पूछा।
सहसा कमरे का वातावरण बदल गया, ‘क्यों, क्या आपको मुझपर विश्वास नहीं है?’ उसका स्वर भर्रा गया।
‘नहीं। मैं वर्ष 1972 में प्राप्त आपका स्वर्ण पदक देखना चाहती हूँ।’ मैंने दोहराया।
‘वह मेरे लिए बहुत मूल्यवान् है, इसलिए मैंने उसे बैंक के लॉकर में रखा है।’ उसने कहा।
मैं भी छोड़नेवाली नहीं थी, ‘किस बैंक में ?’
‘मैं आपको यह सब विवरण क्यों दूँ ?’ मेरी बात से वह चिढ़ सा गया।
तब तक सब कुछ साफ हो गया था। शायद वह भी समझ गया था। सत्कार का समय निकल गया था। मेरी बस का समय हो गया था और मेरे वहाँ से जाने का भी।
द्वार की ओर बढ़ते हुए मैंने उससे कहा, ‘मुझे आपके स्वर्ण पदक व बैंक को जानने की कोई इच्छा नहीं है, यह मेरा काम नहीं है। किंतु मुझे विश्वास है कि वह स्वर्ण पदक आपके पास नहीं है।’
‘आप यह कैसे कह सकती हैं और वह भी इतने विश्वास के साथ?’ अब तक वह आगबबूला हो गया था।
‘क्योंकि सन् 1972 में स्वर्ण पदक मुझे मिला था।’ मैंने धीरे से उदासी भरे स्वर में कहा, ‘और प्रतिवर्ष केवल एक ही स्वर्ण पदक दिया जाता है।’
इसे जानकर वह भौंचक्का रह गया और मेरी ओर एकटक देखने लगा। मैंने उसकी ओर देखा और नम्रतापूर्वक कहा, ‘आप काफी होशियार हैं। अपने काम में प्रवीण हैं। फिर आपको झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है ? इससे आपको क्या मिलेगा ?’
सामने का द्वार मेरे पीछे भड़ाक से बंद हुआ। मुझे यही उत्तर मिलना था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book