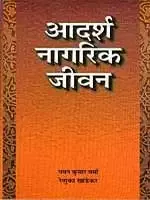|
लेख-निबंध >> आदर्श नागरिक जीवन आदर्श नागरिक जीवनपवन कुमार वर्मा रेणुका खांडेकर
|
424 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है आदर्श नागरिक जीवन...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
भूमिका
अप्रैल 1998 में ‘द ग्रेट इंडियन
मिडिल क्लास’ के आने
के बाद से मैं कई मंचों से भारतीयों को शिक्षित करने की आवश्यकता पर बोलता
रहा हूँ, ताकि इस बड़ी चिंता की ओर ध्यान जा सके कि इस पृथ्वी पर अति
दयनीय लोगों की जो तादाद है, उनमें बड़ी संख्या में लोग भारत में हैं। और
इसके साथ ही सबसे ज्यादा ध्यान निरक्षर लोगों पर दिया जा सके। दुनिया के
मुकाबले भारत में ऐसे लोगों की तादात भी काफी बड़ी है जो मलेरिया और
टी.बी. जैसी बीमारियों से मर जाते हैं। मैंने इस बिंदु को उठाया है कि यह
हमारा खुद का स्वार्थ है, जो स्थिति को बदलने के लिए हमें प्रेरित करने की
कोशिश करे; क्योंकि हम अपने उस जीवन, सुरक्षा और खुशहाली की अनदेखी नहीं
कर सकते जो कि हम अपने व अपने बच्चों के लिए तलाशते हैं।
सवाल-जवाब के सत्रों के दौरान मेरे लिए एक नया रहस्योद्घाटन हुआ। कई सवाल तो ऐसे थे जो यह संकेत देते थे कि एक मध्य वर्गीय नागरिक क्या करे, उसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। कई लोगों ने कहा कि वे अपने जीवन में काफी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं मालूम कि कहाँ से शुरू करें, किसके पास जाएँ, कैसे प्राथमिकताओं का निर्धारण करें। उन लोगों को-खुद को-यह संदेह रहता है कि उनके योगदान का क्या कोई मूल्य होगा ? कहीं पूरी मेहनत बेकार तो नहीं चली जाएगी ?
रेणुका खांडेकर के सामने भी कई नई बातें आईं। उस समय वे महिलाओं की पत्रिका ‘जेना’ का संपादन कर रही थीं। ‘द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास’ के विश्लेषण के आधार पर उन्होंने आम मध्य वर्गीय भारतीय से संबंधित विषयों पर पूरा एक अंक निकाला। यह उनकी अपनी एक छोटी सी कोशिश थी। इस अंक की जो प्रतिक्रिया रेणुकाजी को मिली, उससे वे बहुत ही उत्साहित हुईं। यही वह बात थी जिससे हम दोनों ने एक ऐसी छोटी पुस्तक तैयार करने की शुरूआत की, जो मध्य वर्गीय भारतीयों के लिए एक उम्मीद बन सके और उनमें अपने शहर में रहनेवाले व्यक्ति से कहीं ज्यादा नागरिकों के बीच भागीदारी बढ़ाने का एक जरिया बन सके तथा लोग सही मायने में जागरूक नागरिक बन सकें।
इस पुस्तक की भूमिका की शुरूआत यही है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के बाद भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है जो अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं। इस पुस्तक में एक ऐसे सभ्य नागरिक समाज के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिसमें लोगों के हित समाज की चिंताओं से जुड़े हों।
अंततः, इस पुस्तक में भारत में सरकार, शासन को सुधारने की प्रेरणा निहित है और हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि यह तब तक नहीं हो सकती जब तक नागरिक अपने लिए बेहतर शासन की माँग न करें और यह न जानें कि यह असरदार ढंग से कैसे काम करता है।
यह पुस्तक एक शुरुआत भी है। यह आपको तरीके तो सुझाती है, लेकिन एक संपूर्ण-व्यापक खाका उपलब्ध कराने का दावा नहीं करती। हमें मालूम है कि हम पर आदर्शवादी और अव्यावहारिक होने का आरोप लग सकता है। हमें यह भी पता है कि इस पुस्तक में बताए गए सारे तरीके मध्य वर्ग में छिपी बुराइयों को दूर करने में असरकारक नहीं होंगे। हमारा मानना है कि हमारे सामने जो विकल्प हैं वे बहुत ही सीमित हैं। या तो हम अपना आत्म-विश्लेषण कर अपने दीर्घ हितों को बदल लें या यह स्वीकार कर लें कि ऐसे हित कभी भी फलदायी नहीं होंगे जैसे कि हम मान रहे हैं। इस पुस्तक में इसीलिए सबसे पहले यह बताया गया है कि सबसे पहले हम कम-से-कम कुछ लोगो को तो बदलें। हमारे लिए यह पर्याप्त होगा।
रेणुका खांडेकर के साथ इस पुस्तक को लिखना मुझे बहुत ही आनंददायी लगा है। उनके साथ काम करने के अनुभवों को मैं हमेशा अपने हृदय में सँजोए रखूँगा।
रेणुका खांडेकर और मैं, हम दोनों ही बहुत खुश हैं कि ‘Maximize your life : An action plan for the Indian middle class’ पुस्तक का हिंदी अनुवाद प्रकाशित हो रहा है। जितनी भी पुस्तकें मैंने आज तक लिखी हैं उनमें से मैं समझता हूँ कि प्रस्तुत पुस्तक मध्यम श्रेणी के पाठकों के लिए सर्वाधिक पठनीय है। यह पुस्तक इस बात पर प्रकाश डालती है कि किस प्रकार हम-आप जैसे लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के साथ-साथ अपने बच्चों को भी एक बेहतर भारत प्रदान कर सकते हैं।
अंग्रेजी एक शक्तिशाली भाषा है; परंतु मुझे यह कहते हुए तनिक भी संकोच नहीं है कि इस की पहुँच सीमित है। किसी भी पुस्तक की सर्वाधिक लोकप्रियता के लिए उसे हमारी अपनी भाषा में प्रकाशित करना चाहिए; और सभी भारतीय भाषाओं में हिंदी की पहुँच सर्वाधिक है।
सवाल-जवाब के सत्रों के दौरान मेरे लिए एक नया रहस्योद्घाटन हुआ। कई सवाल तो ऐसे थे जो यह संकेत देते थे कि एक मध्य वर्गीय नागरिक क्या करे, उसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। कई लोगों ने कहा कि वे अपने जीवन में काफी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं मालूम कि कहाँ से शुरू करें, किसके पास जाएँ, कैसे प्राथमिकताओं का निर्धारण करें। उन लोगों को-खुद को-यह संदेह रहता है कि उनके योगदान का क्या कोई मूल्य होगा ? कहीं पूरी मेहनत बेकार तो नहीं चली जाएगी ?
रेणुका खांडेकर के सामने भी कई नई बातें आईं। उस समय वे महिलाओं की पत्रिका ‘जेना’ का संपादन कर रही थीं। ‘द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास’ के विश्लेषण के आधार पर उन्होंने आम मध्य वर्गीय भारतीय से संबंधित विषयों पर पूरा एक अंक निकाला। यह उनकी अपनी एक छोटी सी कोशिश थी। इस अंक की जो प्रतिक्रिया रेणुकाजी को मिली, उससे वे बहुत ही उत्साहित हुईं। यही वह बात थी जिससे हम दोनों ने एक ऐसी छोटी पुस्तक तैयार करने की शुरूआत की, जो मध्य वर्गीय भारतीयों के लिए एक उम्मीद बन सके और उनमें अपने शहर में रहनेवाले व्यक्ति से कहीं ज्यादा नागरिकों के बीच भागीदारी बढ़ाने का एक जरिया बन सके तथा लोग सही मायने में जागरूक नागरिक बन सकें।
इस पुस्तक की भूमिका की शुरूआत यही है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के बाद भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है जो अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं। इस पुस्तक में एक ऐसे सभ्य नागरिक समाज के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिसमें लोगों के हित समाज की चिंताओं से जुड़े हों।
अंततः, इस पुस्तक में भारत में सरकार, शासन को सुधारने की प्रेरणा निहित है और हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि यह तब तक नहीं हो सकती जब तक नागरिक अपने लिए बेहतर शासन की माँग न करें और यह न जानें कि यह असरदार ढंग से कैसे काम करता है।
यह पुस्तक एक शुरुआत भी है। यह आपको तरीके तो सुझाती है, लेकिन एक संपूर्ण-व्यापक खाका उपलब्ध कराने का दावा नहीं करती। हमें मालूम है कि हम पर आदर्शवादी और अव्यावहारिक होने का आरोप लग सकता है। हमें यह भी पता है कि इस पुस्तक में बताए गए सारे तरीके मध्य वर्ग में छिपी बुराइयों को दूर करने में असरकारक नहीं होंगे। हमारा मानना है कि हमारे सामने जो विकल्प हैं वे बहुत ही सीमित हैं। या तो हम अपना आत्म-विश्लेषण कर अपने दीर्घ हितों को बदल लें या यह स्वीकार कर लें कि ऐसे हित कभी भी फलदायी नहीं होंगे जैसे कि हम मान रहे हैं। इस पुस्तक में इसीलिए सबसे पहले यह बताया गया है कि सबसे पहले हम कम-से-कम कुछ लोगो को तो बदलें। हमारे लिए यह पर्याप्त होगा।
रेणुका खांडेकर के साथ इस पुस्तक को लिखना मुझे बहुत ही आनंददायी लगा है। उनके साथ काम करने के अनुभवों को मैं हमेशा अपने हृदय में सँजोए रखूँगा।
रेणुका खांडेकर और मैं, हम दोनों ही बहुत खुश हैं कि ‘Maximize your life : An action plan for the Indian middle class’ पुस्तक का हिंदी अनुवाद प्रकाशित हो रहा है। जितनी भी पुस्तकें मैंने आज तक लिखी हैं उनमें से मैं समझता हूँ कि प्रस्तुत पुस्तक मध्यम श्रेणी के पाठकों के लिए सर्वाधिक पठनीय है। यह पुस्तक इस बात पर प्रकाश डालती है कि किस प्रकार हम-आप जैसे लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के साथ-साथ अपने बच्चों को भी एक बेहतर भारत प्रदान कर सकते हैं।
अंग्रेजी एक शक्तिशाली भाषा है; परंतु मुझे यह कहते हुए तनिक भी संकोच नहीं है कि इस की पहुँच सीमित है। किसी भी पुस्तक की सर्वाधिक लोकप्रियता के लिए उसे हमारी अपनी भाषा में प्रकाशित करना चाहिए; और सभी भारतीय भाषाओं में हिंदी की पहुँच सर्वाधिक है।
पवन कुमार वर्मा
यदि राष्ट्रीय गान गाते समय आपका गला भर आए
या देशभक्ति की पुरानी फिल्मों
के गाने सुनते हुए आँखें डबडबा जाएँ तो आप यह समझ जाएँगे कि इस पुस्तक में
भारतीय जीवन को लेकर हमने कुछ तरीके सुझाने की कोशिश क्यों की है। यह
सोचकर ही मुझे बहुत तकलीफ होती है कि अपनी वर्तमान दशा के मुकाबले भारतीय
जीवन कितना बेहतर हो सकता था।
हम जानते हैं कि अब राष्ट्र निर्माण के उन शुरूआती वर्षों के उत्साह भरे दिन गुजर चुके हैं। वह जमाना था जब हमारा देश मुद्दतों से झुकी हुई गरदन सीधी कर रहा था। आखिर हमने अपनी गिरावट को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? अपने राष्ट्रीय जीवन को पथभ्रष्ट क्यों हो जाने दिया ? लेकिन इसका मतलब यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी है।
हम हर हफ्ते अखबारों-पत्रिकाओं में ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने कुछ अलग कर दिखाया है, क्योंकि उनका मानस एक सच्चे काम को करने का है। ऐसे लोग हमारे लिए जीती-जागती मिसाल हैं, जिनके लिए देश हृदय में है।
हम जानते हैं कि अब राष्ट्र निर्माण के उन शुरूआती वर्षों के उत्साह भरे दिन गुजर चुके हैं। वह जमाना था जब हमारा देश मुद्दतों से झुकी हुई गरदन सीधी कर रहा था। आखिर हमने अपनी गिरावट को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? अपने राष्ट्रीय जीवन को पथभ्रष्ट क्यों हो जाने दिया ? लेकिन इसका मतलब यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी है।
हम हर हफ्ते अखबारों-पत्रिकाओं में ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने कुछ अलग कर दिखाया है, क्योंकि उनका मानस एक सच्चे काम को करने का है। ऐसे लोग हमारे लिए जीती-जागती मिसाल हैं, जिनके लिए देश हृदय में है।
रेणुका खांडेकर
1
चिंतित क्यों ?
यदि समय वाकई बेहद मुश्किल नजर आ रहा हो और
भविष्य एकदम अनिश्चित हो तो इस धारणा को खारिज कर देना चाहिए कि समय और
भविष्य कभी कुछ थे। हमेशा युद्ध होते रहे, विनाश हुआ, अवपात होते रहे,
हमेशा संकट आते रहे।...इतिहास की अमूल्य सीख सिर्फ यही होगी कि समय-समय के
वक्त व्यक्ति किसी का भी सामना कर सकता है, और उसे करना पड़ेगा।
-पैरीज ऑफ मद्रास, ए स्टोरी ऑफ ब्रिटिश
एंटरप्राइजेज इन इंडिया, हिल्टन ब्राउन
एंटरप्राइजेज इन इंडिया, हिल्टन ब्राउन
चिंतित क्यों ?
सचमुच हमें, शिक्षित मध्य वर्ग को, उन
सामाजिक-राजनीतिक कष्टों व
गड़बड़ियों को लेकर चिंतित क्यों होना चाहिए जो हमारे कठोर कर्मशील जीवन
को दूषित किए जा रही हैं ?
क्या शहरी भार खुद अपने में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश नहीं है ? निश्चित रूप से, तब क्या हम खुद अपने आप एक अलग गणतंत्र बनाने के हकदार नहीं हैं-और अपने महत्त्वाकांक्षी निजी कोशिशों से अपने सपनों का भारत, जो हरा-भरा, साफ-सुथरा, खुशहाल-नहीं बना सकते ? सिर्फ तभी...
सिर्फ तभी, जो घृणास्पद हैं उनको निकाल दें, जैसे-बदसूरती, गंदगी गरीबी और जनता के बीच पराजित होनेवाले। उनकी नासमझी, पढ़ने के प्रति अनिच्छा, कम बच्चे पैदा करना, बच्चों को टीके लगवाना, उन्हें नहलाना उनके बाल बनाना....आदि के प्रति हम कितने जिम्मेदार हैं ? देखिए, कैसे वे हमारे जीवन को खराब करते हैं !
फिर भी, जब हम सब ईश्वर की निगाह में एक समान हैं, एक-दूसरे की निगाह में हम समान नहीं हैं। हममें से कुछ साधारण घर में पैदा हुए और बहुत कुछ पाया; जबकि दूसरों के मुकाबले कठोर परिश्रम करने के बावजूद हमें जीवन बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा जाता है।
इसलिए हमारे जैसे लोग जो करते हैं, जो जीवन के बेहतर रास्ते जानते हैं, क्या वे देश के साथ भी हमारी तरह ही करते हैं ? एक-यह अति विशाल है। दो-पृथ्वी की कुल आबादी का सातवाँ हिस्सा यहाँ जन्म लेता है। तीन-और जो हम सबके लिए सबसे ज्यादा घातक है, वह यह कि सबसे बड़ा निम्न वर्ग, गरीबी यहाँ है।
ये तीन जो विकराल विषमताएँ व समस्याएँ हैं, इनसे हमें उबरना चाहिए और इसकी कोशिशें हमारी सामूहिक परिकल्पना के यहीं कहीं हैं।
यह सोचना सबसे ज्यादा आत्ममोहक (और बाद में आत्मनिंदक) होगा कि हम यह उम्मीद लगा लें कि मशीन का कोई देवता उतरकर आएगा और समस्याएँ हल कर देगा, जैसाकि प्राचीन यूनानी नाटकों में हुआ करता था और यह हम खुद भी अपने लोक-साहित्य मिथकों और सिनेमाओं में भी पाते हैं। सच्चाई यह है कि हमारे पास सीमित विकल्प हैं-और इस सच्चाई को हमने बहुत ही जल्दी अच्छी तरह से समझ लिया है-
1. कोई ऐसा मसीहा या नेता नहीं है जो अचानक आकर जादुई ढंग से रात भर में सबकुछ बदल डाले।
2. चीन या सोवियत संघ में जो महाक्रांति हुई और उससे हुई उछल-पुथल के बाद वहाँ कायापलट हो गई, वैसी यहाँ कोई राजनीतिक क्रांति अभी नहीं होने वाली और न ही समाज के ढाँचे में कोई भूकंप जैसा बदलाव आने वाला है। इसलिए इस मामले में कुछ भी करना हमारे लिए अनावश्यक ही है।
3. अर्थशास्त्र का मशहूर परिस्रवण सिद्धांत काम नहीं करेगा। बड़ी संख्या में गरीबों को पर्याप्त आर्थिक फायदे पहुँचाने के लिए व्यवस्था खुद पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकेगी। हालाँकि जो आशावादी आर्थिक मॉडल है उसका सीधा सा तथ्य यह है कि सन् 2025 तक मध्य वर्ग-जो कि हम हैं-की तादाद ही लगभग पचास करोड़ तक पहुँच जाएगी तथा गरीबों व अति पिछड़ों (वंचित तबका) की तादाद लगभग साठ करोड़ होगी।
4. टेक्नोलॉजी में कोई अचानक ही क्रांति नहीं आ जाएगी, जैसे कि मोटापा कम करने की ऐसी गोली हो जो बिना डाइटिंग के ही मोटापा कम कर दे। इसलिए भारत की समस्याओं को हमारे प्रयासों के बिना हल नहीं किया जा सकता।
तो इस तरह क्या होने जा रहा है ? क्या यह किसी सभ्यता के अंत की शुरूआत है ? हममें से ज्यादा लोग जो उम्मीद किए बैठे हैं, वास्तव में उससे भी पहले संकट के लक्षण बहुत ही जल्दी सामने आने लग जाएँगे, इसपर विश्वास नहीं होता। थोड़े दिन के लिए नैरोबी चले जाइए। बेहद अमीरी है वहाँ; होटल, कैसिनो, रेस्तराँ, बड़े-बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आलीशान इमारतें, घर-बाग-सब हैं। लेकिन यदि वहाँ शाम साढ़े छह बजे के बाद आपको बाहर निकलना है तो अपने साथ हथियारबंद सुरक्षा गार्ड रखने की जरूरत होगी।
ऐसा इसलिए है, क्योंकि केन्या में 47 फीसदी लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। तीस साल पहले नैरोबी के संपन्न नागरिकों ने सोचा था कि ये लोग उनकी जिंदगी को प्रभावित नहीं करेंगे। अब ये लोग कह रहें हैं कि खुद की धन-दौलत होते हुए भी हम कैदियों की तरह रह रहे हैं। गरीबों को पीठ दिखाते हुए इन अमीरों ने एक ऐसा समाज बना दिया, जिसमें अब जंगलराज कायम है।
दक्षिण अफ्रीका में भी यही सब हो रहा है, जहाँ 38 से 40 फीसदी आबादी बेरोजगारों की है। हालाँकि जोहांसबर्ग में कुछ खुशहाल लोग हो सकते हैं। उस शहर में या देश में कहीं भी एक अच्छी बात जो है, वह है सुरक्षा, सेवाएँ।
इसलिए पहली सच्चाई यह जानना है कि हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है उससे हम अपने जीवन को अलग नहीं कर सकते। और वह जो भी हो ! इन तथ्यों पर गौर करें-
1. हमारे देश में तकरीबन तीस करोड़ लोग रोजाना रात को भूखे सोते हैं। यह तादाद अमेरिका, कनाडा और पश्चिम यूरोप के देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। यह योजना आयोग का एक आँकड़ा है और यह एकदम उस पैमाने से आया है, जिसे गरीबी रेखा के नाम से जाना जाता है।
2. गरीबी रेखा के आसपास ही तीस करोड़ लोग और हैं। एक रोजी-रोटी की तलाश में मर जाता है, एक किसी हादसे या बीमारी से-और इस तरह पूरा-का-पूरा परिवार गरीबी रेखा से नीचे चला जाता है।
3. इस प्रकार करीब एक अरब की आबादीवाले राष्ट्र में हम पैंसठ करोड़ लोग अमानवीय हालात में जकड़े हुए हैं। पैंसठ करोड़ की यह तादाद पूरे यूरोप व अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा है।
4. यूनीसेफ की रिपोर्ट बताती है कि सन् 2000 में भारत दुनिया का सर्वाधिक निरक्षर देश होगा, जो कि अमेरिका और कनाडा की कुल आबादी से ज्यादा हैं।
5. पाँच साल से कम उम्र के साढ़े सात करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इसका मतलब यह है कि सारे भारतीय बच्चों में से आधे से ज्यादा कुपोषण के शिकार हैं और यह दर इथोपिया से भी कहीं ज्यादा बदतर है। इथोपिया चार करोड़ नब्बे लाख की आबादीवाला वह देश है जिसका युद्ध व बहु औपनिवेशिक शोषण का दर्दनाक इतिहास रहा है।
6. हर साल बीस लाख भारतीय बच्चे (शिशु) अपने जन्म का पहला साल पूरा होने से पहले ही मर जाते हैं। यह आँकड़ा मॉरीशस की आबादी के दुगुने से भी ज्यादा है।
7. भारत में हर तीसरे मिनट में एक बच्चे की मौत डायरिया (अतिसार) जैसी साध्य बीमारी के कारण हो जाती है।
8. करीब 60 फीसदी लोगों के पास बिजली नहीं है।
9. 75 फीसदी लोगों को नल का पानी उपलब्ध नहीं है।
10. करीब 60 फीसदी लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए पक्के घर नहीं हैं।
11. यदि ये तथ्य वाकई इतने जबरदस्त हैं तो क्यों नहीं हम परेशान या चिंतित हों, या इन पर गौर करें ?
मध्य वर्ग के ज्यादातर लोग अपने आपको शिक्षित, स्पष्ट कहनेवाला, परिष्कृत, सौम्य मानते हैं, जो पाँच हजार साल से चली आ रही सभ्यता के अंतिम हिस्से हैं। तब ऐसा क्यों है कि हम गौर नहीं करते ? ऐसा क्यों है कि हम अपने में इस बात से संतुष्ट हो गए हैं कि ये जो आँकड़े हैं, चमत्कारिक ढंग से ये भी सच होंगे कि वे किसी दूसरी जगह के लोग हैं, दूसरे देश के हैं, दूसरे ग्रह के हैं, और अन्यत्र कहीं के भी हों, लेकिन भारत ? दरअसल इन आँकड़ों का अब हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रह गया है। हमारे जैसे लोगों के लिए भारत के बारे में सच्चाई सिर्फ यही है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है (जो कि यह है भी), जो दुनिया की सबसे ज्यादा कुशल मानव शक्ति से युक्त है (और संख्या में वाकई यह है), जिसने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई मोरचों पर बड़ी सफलताएँ हासिल की हैं (यह भी सही है) और यह वह राष्ट्र है जो दुनिया के सबसे बड़े मध्य वर्ग से खुश है।
छवि बनानेवाले ऐसे विज्ञापनों की वजह से ही शिक्षित भारतीय मध्य वर्ग ने सिर्फ ध्यान देना बंद कर दिया है। आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि यह सच हमें ठीक हमारे दरवाजे पर ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है-
1. सरकारी आँकड़ों के अनुसार दिल्ली के 40 फीसदी लोग झुग्गियों में रहते हैं।
2. भारत का पहला शहर कहे जानेवाले मुंबई की आधी आबादी झोंपड़ बस्तियों में रहती है। विशाल मध्य वर्ग के भारत का इससे ज्यादा भयानक मजाक और क्या होगा कि मीडिया, विज्ञापन और वाणिज्य जैसे क्षेत्रों में काम करनेवाले लोग और अपने को शिक्षित, स्पष्ट बोलनेवाला समझनेवाले लोग खुद कितने बड़े धोखे में रहते हैं। यही लोग मुंबई को न्यूयॉर्क जैसा मानते हैं। मुंबई के बारे में एक बात और कही जाती है-‘हमारे पास हर चीज के लिए एक व्यवस्था है-खाने के डिब्बों से लेकर पुरानी बजबत की गई कारों को ठीक करने बंदी।’ सच्चाई यह है कि मुंबई इस धरती का सर्वाधिक दूषित और बदसूरत शहर है, जहाँ लोग आसानी से फ्लैट नहीं खरीद सकते और जिनकी आधी से ज्यादा जिंदगी उपनगरों से आने-जाने में गुजर जाती है।
3. भारत की राजधानी दिल्ली में करीब 35 फीसदी लोग खुले में शौच जाते हैं।
4. राजधानी दिल्ली में तकरीबन 40 फीसदी लोग निरक्षर हैं।
5. दिल्ली में करीब पंद्रह सौ टन कचरा रोजाना बिना उठे रह जाता है। भारत के दूसरे बड़े शहरों में भी तकरीबन यही स्थिति है।
लेकिन मध्य वर्गीय भारत वह चीज दर्ज नहीं करता है जो कोई भी विदेशी दर्ज करना नहीं छोड़ता है। और वह यह कि हमारे चारों ओर बहुत कुछ गलत हो रहा है, जिसमें तुरंत सुधार लाने की जरूरत है।
हमारा एक यह दृढ़ विश्वास रहा है कि अत्यधिक आबादी ही सिर्फ एक बड़ा दोष है। यदि अति पिछड़ों-निम्न वर्ग के लोगों की तादाद एकदम घट जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इस बारे में कुछ करने के लिए हमें करना क्या होगा ? यदि लोकतंत्र में लाखों की तादाद में गरीबों की जबरन नसबंदी करना संभव है तो हममें से कई इसके लिए सहमत हो जाएँगे कि यही सबसे बेहतर नीति है। लेकिन समस्या यह है कि ऐसी नीति बनाना, लागू करना संभव नहीं है। एक बार पहले ऐसी कोशिश की जा चुकी है, लेकिन सफल नहीं हुई।
न ही यह सर्वश्रेष्ठ नीति है। इनसानों के साथ वस्तुओं की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता। भारत की अत्यधिक आबादी का असली जवाब प्राथमिक शिक्षा के प्रसार, स्वास्थ्य की देखभाल और महिला साक्षरता में मिलता है। बुनियादी शिक्षा के अभाव में बहुसंख्य भारतीय अपने दीर्घकालिक हितों के लिए फैसला लेने में न सिर्फ सक्षम होंगे बल्कि सरकार की परिवार नियोजन नीति की जरूरत के प्रचार को भी नहीं समझ पाएँगे।
लेकिन जन शिक्षा हमें तत्काल ही कोई परिणाम नहीं दे देगी, न ही हमारे जैसे लोग यह मानेंगे कि यह भी एक कारगर तरीका है। हम हर चीज तत्काल चाहते हैं और हम यह सिर्फ अपने लिए ही चाहते हैं।
हममें से अधिकतर लोगों का यह मानना है कि हर चीज अथवा समस्या का आदर्श हल यही है कि हम अपनी ही दुनिया के चारों ओर एक गढ़-सा बना लें। हममें से कुछ बहादुर लोग इसकी कोशिश भी करते हैं। हम लाइनमैन को रिश्वत देने के इच्छुक रहते हैं, ताकि हमें बिजली मिल जाए। पानी की मुख्य लाइन में बूस्टर लगाकर अपना टैंक भर लेने की कोशिश हमारी रहती है। अगर घर के दरवाजे के बाहर कूड़ा पड़ा हो तो उसकी हमें कोई चिंता नहीं, बस हमारा अपना घर साफ-सुथरा रहना चाहिए।
लेकिन सच्चाई यह है कि इस तरह लोग जो अपने ‘निजी किले’ तैयार कर लेते हैं वे बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाते। ऐसे छोटे, टापू पूरी व्यवस्था के साथ खुद डूबते जा रहे हैं। ऐसे ‘निजी किलों’ अथवा ‘टापुओं’ की संख्या बढ़ सकती है; लेकिन पूरी तरह बेअसर व्यवस्था उनको नीचे से काटती हुई खत्म करती जा रही है। इसलिए कोई समाधान नहीं है। लेकिन हमारे चारों ओर जो कुछ घटित हो रहा है, उसके बारे में परेशानी और चिंता है। इसके लिए अत्यावश्यक जरूरत प्रतिबद्ध होने की है। ‘बाशिंदों’ से पूरी तरह ‘नागरिक’ बनने की जरूरत है। इस प्रतिज्ञा के लिए किसी नाटकीय बलिदान की जरूरत नहीं है। किसी को भी पूर्णकालिक सामाजिक कार्यकर्ता बनने की आवश्यकता नहीं है। न ही हममें से किसी को महात्मा बनने की जरूरत है।
क्या शहरी भार खुद अपने में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश नहीं है ? निश्चित रूप से, तब क्या हम खुद अपने आप एक अलग गणतंत्र बनाने के हकदार नहीं हैं-और अपने महत्त्वाकांक्षी निजी कोशिशों से अपने सपनों का भारत, जो हरा-भरा, साफ-सुथरा, खुशहाल-नहीं बना सकते ? सिर्फ तभी...
सिर्फ तभी, जो घृणास्पद हैं उनको निकाल दें, जैसे-बदसूरती, गंदगी गरीबी और जनता के बीच पराजित होनेवाले। उनकी नासमझी, पढ़ने के प्रति अनिच्छा, कम बच्चे पैदा करना, बच्चों को टीके लगवाना, उन्हें नहलाना उनके बाल बनाना....आदि के प्रति हम कितने जिम्मेदार हैं ? देखिए, कैसे वे हमारे जीवन को खराब करते हैं !
फिर भी, जब हम सब ईश्वर की निगाह में एक समान हैं, एक-दूसरे की निगाह में हम समान नहीं हैं। हममें से कुछ साधारण घर में पैदा हुए और बहुत कुछ पाया; जबकि दूसरों के मुकाबले कठोर परिश्रम करने के बावजूद हमें जीवन बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा जाता है।
इसलिए हमारे जैसे लोग जो करते हैं, जो जीवन के बेहतर रास्ते जानते हैं, क्या वे देश के साथ भी हमारी तरह ही करते हैं ? एक-यह अति विशाल है। दो-पृथ्वी की कुल आबादी का सातवाँ हिस्सा यहाँ जन्म लेता है। तीन-और जो हम सबके लिए सबसे ज्यादा घातक है, वह यह कि सबसे बड़ा निम्न वर्ग, गरीबी यहाँ है।
ये तीन जो विकराल विषमताएँ व समस्याएँ हैं, इनसे हमें उबरना चाहिए और इसकी कोशिशें हमारी सामूहिक परिकल्पना के यहीं कहीं हैं।
यह सोचना सबसे ज्यादा आत्ममोहक (और बाद में आत्मनिंदक) होगा कि हम यह उम्मीद लगा लें कि मशीन का कोई देवता उतरकर आएगा और समस्याएँ हल कर देगा, जैसाकि प्राचीन यूनानी नाटकों में हुआ करता था और यह हम खुद भी अपने लोक-साहित्य मिथकों और सिनेमाओं में भी पाते हैं। सच्चाई यह है कि हमारे पास सीमित विकल्प हैं-और इस सच्चाई को हमने बहुत ही जल्दी अच्छी तरह से समझ लिया है-
1. कोई ऐसा मसीहा या नेता नहीं है जो अचानक आकर जादुई ढंग से रात भर में सबकुछ बदल डाले।
2. चीन या सोवियत संघ में जो महाक्रांति हुई और उससे हुई उछल-पुथल के बाद वहाँ कायापलट हो गई, वैसी यहाँ कोई राजनीतिक क्रांति अभी नहीं होने वाली और न ही समाज के ढाँचे में कोई भूकंप जैसा बदलाव आने वाला है। इसलिए इस मामले में कुछ भी करना हमारे लिए अनावश्यक ही है।
3. अर्थशास्त्र का मशहूर परिस्रवण सिद्धांत काम नहीं करेगा। बड़ी संख्या में गरीबों को पर्याप्त आर्थिक फायदे पहुँचाने के लिए व्यवस्था खुद पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकेगी। हालाँकि जो आशावादी आर्थिक मॉडल है उसका सीधा सा तथ्य यह है कि सन् 2025 तक मध्य वर्ग-जो कि हम हैं-की तादाद ही लगभग पचास करोड़ तक पहुँच जाएगी तथा गरीबों व अति पिछड़ों (वंचित तबका) की तादाद लगभग साठ करोड़ होगी।
4. टेक्नोलॉजी में कोई अचानक ही क्रांति नहीं आ जाएगी, जैसे कि मोटापा कम करने की ऐसी गोली हो जो बिना डाइटिंग के ही मोटापा कम कर दे। इसलिए भारत की समस्याओं को हमारे प्रयासों के बिना हल नहीं किया जा सकता।
तो इस तरह क्या होने जा रहा है ? क्या यह किसी सभ्यता के अंत की शुरूआत है ? हममें से ज्यादा लोग जो उम्मीद किए बैठे हैं, वास्तव में उससे भी पहले संकट के लक्षण बहुत ही जल्दी सामने आने लग जाएँगे, इसपर विश्वास नहीं होता। थोड़े दिन के लिए नैरोबी चले जाइए। बेहद अमीरी है वहाँ; होटल, कैसिनो, रेस्तराँ, बड़े-बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आलीशान इमारतें, घर-बाग-सब हैं। लेकिन यदि वहाँ शाम साढ़े छह बजे के बाद आपको बाहर निकलना है तो अपने साथ हथियारबंद सुरक्षा गार्ड रखने की जरूरत होगी।
ऐसा इसलिए है, क्योंकि केन्या में 47 फीसदी लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। तीस साल पहले नैरोबी के संपन्न नागरिकों ने सोचा था कि ये लोग उनकी जिंदगी को प्रभावित नहीं करेंगे। अब ये लोग कह रहें हैं कि खुद की धन-दौलत होते हुए भी हम कैदियों की तरह रह रहे हैं। गरीबों को पीठ दिखाते हुए इन अमीरों ने एक ऐसा समाज बना दिया, जिसमें अब जंगलराज कायम है।
दक्षिण अफ्रीका में भी यही सब हो रहा है, जहाँ 38 से 40 फीसदी आबादी बेरोजगारों की है। हालाँकि जोहांसबर्ग में कुछ खुशहाल लोग हो सकते हैं। उस शहर में या देश में कहीं भी एक अच्छी बात जो है, वह है सुरक्षा, सेवाएँ।
इसलिए पहली सच्चाई यह जानना है कि हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है उससे हम अपने जीवन को अलग नहीं कर सकते। और वह जो भी हो ! इन तथ्यों पर गौर करें-
1. हमारे देश में तकरीबन तीस करोड़ लोग रोजाना रात को भूखे सोते हैं। यह तादाद अमेरिका, कनाडा और पश्चिम यूरोप के देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। यह योजना आयोग का एक आँकड़ा है और यह एकदम उस पैमाने से आया है, जिसे गरीबी रेखा के नाम से जाना जाता है।
2. गरीबी रेखा के आसपास ही तीस करोड़ लोग और हैं। एक रोजी-रोटी की तलाश में मर जाता है, एक किसी हादसे या बीमारी से-और इस तरह पूरा-का-पूरा परिवार गरीबी रेखा से नीचे चला जाता है।
3. इस प्रकार करीब एक अरब की आबादीवाले राष्ट्र में हम पैंसठ करोड़ लोग अमानवीय हालात में जकड़े हुए हैं। पैंसठ करोड़ की यह तादाद पूरे यूरोप व अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा है।
4. यूनीसेफ की रिपोर्ट बताती है कि सन् 2000 में भारत दुनिया का सर्वाधिक निरक्षर देश होगा, जो कि अमेरिका और कनाडा की कुल आबादी से ज्यादा हैं।
5. पाँच साल से कम उम्र के साढ़े सात करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इसका मतलब यह है कि सारे भारतीय बच्चों में से आधे से ज्यादा कुपोषण के शिकार हैं और यह दर इथोपिया से भी कहीं ज्यादा बदतर है। इथोपिया चार करोड़ नब्बे लाख की आबादीवाला वह देश है जिसका युद्ध व बहु औपनिवेशिक शोषण का दर्दनाक इतिहास रहा है।
6. हर साल बीस लाख भारतीय बच्चे (शिशु) अपने जन्म का पहला साल पूरा होने से पहले ही मर जाते हैं। यह आँकड़ा मॉरीशस की आबादी के दुगुने से भी ज्यादा है।
7. भारत में हर तीसरे मिनट में एक बच्चे की मौत डायरिया (अतिसार) जैसी साध्य बीमारी के कारण हो जाती है।
8. करीब 60 फीसदी लोगों के पास बिजली नहीं है।
9. 75 फीसदी लोगों को नल का पानी उपलब्ध नहीं है।
10. करीब 60 फीसदी लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए पक्के घर नहीं हैं।
11. यदि ये तथ्य वाकई इतने जबरदस्त हैं तो क्यों नहीं हम परेशान या चिंतित हों, या इन पर गौर करें ?
मध्य वर्ग के ज्यादातर लोग अपने आपको शिक्षित, स्पष्ट कहनेवाला, परिष्कृत, सौम्य मानते हैं, जो पाँच हजार साल से चली आ रही सभ्यता के अंतिम हिस्से हैं। तब ऐसा क्यों है कि हम गौर नहीं करते ? ऐसा क्यों है कि हम अपने में इस बात से संतुष्ट हो गए हैं कि ये जो आँकड़े हैं, चमत्कारिक ढंग से ये भी सच होंगे कि वे किसी दूसरी जगह के लोग हैं, दूसरे देश के हैं, दूसरे ग्रह के हैं, और अन्यत्र कहीं के भी हों, लेकिन भारत ? दरअसल इन आँकड़ों का अब हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रह गया है। हमारे जैसे लोगों के लिए भारत के बारे में सच्चाई सिर्फ यही है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है (जो कि यह है भी), जो दुनिया की सबसे ज्यादा कुशल मानव शक्ति से युक्त है (और संख्या में वाकई यह है), जिसने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई मोरचों पर बड़ी सफलताएँ हासिल की हैं (यह भी सही है) और यह वह राष्ट्र है जो दुनिया के सबसे बड़े मध्य वर्ग से खुश है।
छवि बनानेवाले ऐसे विज्ञापनों की वजह से ही शिक्षित भारतीय मध्य वर्ग ने सिर्फ ध्यान देना बंद कर दिया है। आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि यह सच हमें ठीक हमारे दरवाजे पर ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है-
1. सरकारी आँकड़ों के अनुसार दिल्ली के 40 फीसदी लोग झुग्गियों में रहते हैं।
2. भारत का पहला शहर कहे जानेवाले मुंबई की आधी आबादी झोंपड़ बस्तियों में रहती है। विशाल मध्य वर्ग के भारत का इससे ज्यादा भयानक मजाक और क्या होगा कि मीडिया, विज्ञापन और वाणिज्य जैसे क्षेत्रों में काम करनेवाले लोग और अपने को शिक्षित, स्पष्ट बोलनेवाला समझनेवाले लोग खुद कितने बड़े धोखे में रहते हैं। यही लोग मुंबई को न्यूयॉर्क जैसा मानते हैं। मुंबई के बारे में एक बात और कही जाती है-‘हमारे पास हर चीज के लिए एक व्यवस्था है-खाने के डिब्बों से लेकर पुरानी बजबत की गई कारों को ठीक करने बंदी।’ सच्चाई यह है कि मुंबई इस धरती का सर्वाधिक दूषित और बदसूरत शहर है, जहाँ लोग आसानी से फ्लैट नहीं खरीद सकते और जिनकी आधी से ज्यादा जिंदगी उपनगरों से आने-जाने में गुजर जाती है।
3. भारत की राजधानी दिल्ली में करीब 35 फीसदी लोग खुले में शौच जाते हैं।
4. राजधानी दिल्ली में तकरीबन 40 फीसदी लोग निरक्षर हैं।
5. दिल्ली में करीब पंद्रह सौ टन कचरा रोजाना बिना उठे रह जाता है। भारत के दूसरे बड़े शहरों में भी तकरीबन यही स्थिति है।
लेकिन मध्य वर्गीय भारत वह चीज दर्ज नहीं करता है जो कोई भी विदेशी दर्ज करना नहीं छोड़ता है। और वह यह कि हमारे चारों ओर बहुत कुछ गलत हो रहा है, जिसमें तुरंत सुधार लाने की जरूरत है।
हमारा एक यह दृढ़ विश्वास रहा है कि अत्यधिक आबादी ही सिर्फ एक बड़ा दोष है। यदि अति पिछड़ों-निम्न वर्ग के लोगों की तादाद एकदम घट जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इस बारे में कुछ करने के लिए हमें करना क्या होगा ? यदि लोकतंत्र में लाखों की तादाद में गरीबों की जबरन नसबंदी करना संभव है तो हममें से कई इसके लिए सहमत हो जाएँगे कि यही सबसे बेहतर नीति है। लेकिन समस्या यह है कि ऐसी नीति बनाना, लागू करना संभव नहीं है। एक बार पहले ऐसी कोशिश की जा चुकी है, लेकिन सफल नहीं हुई।
न ही यह सर्वश्रेष्ठ नीति है। इनसानों के साथ वस्तुओं की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता। भारत की अत्यधिक आबादी का असली जवाब प्राथमिक शिक्षा के प्रसार, स्वास्थ्य की देखभाल और महिला साक्षरता में मिलता है। बुनियादी शिक्षा के अभाव में बहुसंख्य भारतीय अपने दीर्घकालिक हितों के लिए फैसला लेने में न सिर्फ सक्षम होंगे बल्कि सरकार की परिवार नियोजन नीति की जरूरत के प्रचार को भी नहीं समझ पाएँगे।
लेकिन जन शिक्षा हमें तत्काल ही कोई परिणाम नहीं दे देगी, न ही हमारे जैसे लोग यह मानेंगे कि यह भी एक कारगर तरीका है। हम हर चीज तत्काल चाहते हैं और हम यह सिर्फ अपने लिए ही चाहते हैं।
हममें से अधिकतर लोगों का यह मानना है कि हर चीज अथवा समस्या का आदर्श हल यही है कि हम अपनी ही दुनिया के चारों ओर एक गढ़-सा बना लें। हममें से कुछ बहादुर लोग इसकी कोशिश भी करते हैं। हम लाइनमैन को रिश्वत देने के इच्छुक रहते हैं, ताकि हमें बिजली मिल जाए। पानी की मुख्य लाइन में बूस्टर लगाकर अपना टैंक भर लेने की कोशिश हमारी रहती है। अगर घर के दरवाजे के बाहर कूड़ा पड़ा हो तो उसकी हमें कोई चिंता नहीं, बस हमारा अपना घर साफ-सुथरा रहना चाहिए।
लेकिन सच्चाई यह है कि इस तरह लोग जो अपने ‘निजी किले’ तैयार कर लेते हैं वे बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाते। ऐसे छोटे, टापू पूरी व्यवस्था के साथ खुद डूबते जा रहे हैं। ऐसे ‘निजी किलों’ अथवा ‘टापुओं’ की संख्या बढ़ सकती है; लेकिन पूरी तरह बेअसर व्यवस्था उनको नीचे से काटती हुई खत्म करती जा रही है। इसलिए कोई समाधान नहीं है। लेकिन हमारे चारों ओर जो कुछ घटित हो रहा है, उसके बारे में परेशानी और चिंता है। इसके लिए अत्यावश्यक जरूरत प्रतिबद्ध होने की है। ‘बाशिंदों’ से पूरी तरह ‘नागरिक’ बनने की जरूरत है। इस प्रतिज्ञा के लिए किसी नाटकीय बलिदान की जरूरत नहीं है। किसी को भी पूर्णकालिक सामाजिक कार्यकर्ता बनने की आवश्यकता नहीं है। न ही हममें से किसी को महात्मा बनने की जरूरत है।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book