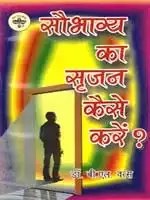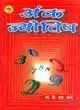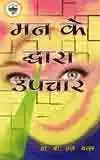|
विविध >> सौभाग्य का सृजन कैसे करें सौभाग्य का सृजन कैसे करेंबी. एल. वत्स
|
348 पाठक हैं |
||||||
ज्योतिषीय आधार पर पूर्वकर्मों के दोषों की जानकारी प्राप्त करके अपने सौभाग्य का सृजन करें...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्राक्कथन
मानव जीवन विधाता का श्रेष्ठतम उपहार है किन्तु इसको व्यर्थ ही बिता देने
का यत्र-तत्र उपक्रम देखकर कोई भी सहृदय व्यथित हो उठेगा। वह ऐसे उपाय
खोजना चाहेगा जिससे मानव-जीवन सार्थक बनाया जा सके।। भगवान् बुद्ध की
करुणा, आदि कवि वाल्मीकि की ‘क्रौञ्च-वध’ के समय उपजी पीड़ा
तथा कवियों की वेदना इसी कोटि की रही है। उनमें पर-दुःख कातरता, सहृदयता,
प्रेम सहिष्णुता का अतिरेक हुआ करता है। अपने चारों ओर पतन-पराभाव को
देखकर मन में यह विचार उठा कि जब हमारे पास अकूत अनुभवों की निधि
विद्यमान है तो क्यों न सौभाग्य के सृजन का उपाय खोजा जाय ? और जन-साधारण
को यह बताया जाय कि जो दुःख हम सह रहे हैं वे हमारे ही संचित, प्रारब्ध
एवं क्रियमाण कर्मों का प्रतिफल है। ज्योतिष के आधार पर जन्म-कुण्डली
देखकर ज्ञात हो जाता है कि व्यक्ति के ऊपर वर्तमान जन्म में किन-किन ऋणों
का बार है ? इन्हें निश्चित अनुष्ठान द्वारा उतारकर वह सुखी, सम्पन्न,
निरोग और आनन्दमय जीवन जी सकता है और पथ में आने वाली चट्टानों जैसी
बाधाओं से मुक्ति पा सकता है। इस कृति में अनेकों अनुभवों को सँजोये हुए
ऐसा मार्ग सुझाया गया है जिससे सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है।
‘सौभाग्य का सृजन कैसे करें ?’
पतन पराभव की पीड़ा के लिए संजीवनी है।
इस कृति को पाठकों तक पहुँचाने में प्रारंभ से अन्त तक भगवती पॉकेट बुक्स, आगरा के संचालक श्री राजीव अग्रवाल की अग्रणी भूमिका रही है। लेखक उनका ह्रदय से आभारी है। जिन विद्वानों एवं प्रकाशकों की कृतियों का सहारा सिद्धान्तों की पुष्टि हेतु लिया गया है, उनका वह कृतज्ञ है। डॉ. निशीथ वत्स ने पुस्तक की पाण्डुलिपि तैयार करने में लेखक की महती सहायता की है, वह उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है।
आशा है पाठक इसका ललककर स्वागत करेंगे।
पतन पराभव की पीड़ा के लिए संजीवनी है।
इस कृति को पाठकों तक पहुँचाने में प्रारंभ से अन्त तक भगवती पॉकेट बुक्स, आगरा के संचालक श्री राजीव अग्रवाल की अग्रणी भूमिका रही है। लेखक उनका ह्रदय से आभारी है। जिन विद्वानों एवं प्रकाशकों की कृतियों का सहारा सिद्धान्तों की पुष्टि हेतु लिया गया है, उनका वह कृतज्ञ है। डॉ. निशीथ वत्स ने पुस्तक की पाण्डुलिपि तैयार करने में लेखक की महती सहायता की है, वह उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है।
आशा है पाठक इसका ललककर स्वागत करेंगे।
डॉ.बी.एल.वत्स
1
कर्मबन्धन और कर्म-मुक्ति
बहु बन्धन से बाँधिया, एक बिचारा जीव।
जीव बिचारा क्या करे, जो छुड़ावे पीव ?
जीव बिचारा क्या करे, जो छुड़ावे पीव ?
सन्त कबीर
महाकाल ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की तब कर्म का जाल बनाया। ये कर्म दो
प्रकार के हैं—एक शुभ, दूसरा अशुभ। ये दोनों कर्म बड़ी बेड़ियाँ
हैं। इस बेड़ी ने समस्त सृष्टि को बाँध लिया है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म
करता है उसे सम्पत्ति एवं वैभव प्राप्त होते हैं। मरणोपरान्त उसे बैकुण्ठ
मिलता है। इस पुण्य का अन्तिम फल चार प्रकार की मुक्ति है—1.
सारूप्य, 2. सालोक्य, 3. सामीप्य, और 4. सायुज्य।
सारुप्य मुक्ति में अपने इष्ट-देव का प्रकट रूप प्राप्त होता है, सालोक्य मुक्ति में अपने इष्ट-देव के लोक में साधक को वास मिलता है, सामीप्य मुक्ति में अपने इष्ट देव के निकट रहने का सुख प्राप्त हो जाता है और सायुज्य मुक्ति में साधक अपने इष्ट के लक्ष्य स्वरूप मिलकर एक हो जाता है। कर्म के अन्य तीन भेद भी बतलाये जाते हैं—कर्म, अकर्म, और विकर्म।
कर्म तो मनुष्य को करना उचित है। अकर्म से दूर भागना और विकर्म से मनुष्य अपने को मुक्त करता और भाग्यवान बनता है। जो शास्त्रानुसार कर्म ईश्वर निमित्त किया जाता है वह विधि है, दूसरा अकर्म जिससे लोक-परलोक में कहीं सुख की प्राप्ति नहीं होती इसे ही शास्त्र में ‘निषेध’ कहते हैं। ये अकर्म ईश्वर के विरुद्ध हैं। विकर्म उसको कहते हैं जिनके करने से कर्म से छूटें। बन्धन के पाश इन्हीं के करने से टूटते हैं और लाभ होता है।
कर्म के अन्य तीन भेद बतलाये जाते हैं—1. संचित, 2. प्रारब्ध, और 3. क्रियमाण।
सारुप्य मुक्ति में अपने इष्ट-देव का प्रकट रूप प्राप्त होता है, सालोक्य मुक्ति में अपने इष्ट-देव के लोक में साधक को वास मिलता है, सामीप्य मुक्ति में अपने इष्ट देव के निकट रहने का सुख प्राप्त हो जाता है और सायुज्य मुक्ति में साधक अपने इष्ट के लक्ष्य स्वरूप मिलकर एक हो जाता है। कर्म के अन्य तीन भेद भी बतलाये जाते हैं—कर्म, अकर्म, और विकर्म।
कर्म तो मनुष्य को करना उचित है। अकर्म से दूर भागना और विकर्म से मनुष्य अपने को मुक्त करता और भाग्यवान बनता है। जो शास्त्रानुसार कर्म ईश्वर निमित्त किया जाता है वह विधि है, दूसरा अकर्म जिससे लोक-परलोक में कहीं सुख की प्राप्ति नहीं होती इसे ही शास्त्र में ‘निषेध’ कहते हैं। ये अकर्म ईश्वर के विरुद्ध हैं। विकर्म उसको कहते हैं जिनके करने से कर्म से छूटें। बन्धन के पाश इन्हीं के करने से टूटते हैं और लाभ होता है।
कर्म के अन्य तीन भेद बतलाये जाते हैं—1. संचित, 2. प्रारब्ध, और 3. क्रियमाण।
पहला—
संचित कर्म उस कर्म को कहते हैं जो हजारों जन्म से बराबर
जीव
के साथ चला आता है। ऋण अदा करने का समय नहीं मिला और ऋण सिर पर चढ़ता चला
गया।
दूसरा—
प्रारब्ध कर्म वह है जिसे भाग्य कहते हैं। इसी प्रारब्ध
कर्म
के अनुसार मानव शरीर प्राप्त हुआ है अर्थात् अपने पूर्व कर्मानुसार ही यह
शरीर प्राप्त हुआ है। जब यह जीव अपने पूर्व शरीर को छोड़ता है तब
‘अहम्’ बोलता है। ‘अहम’ का अर्थ
है—‘मैं हूँ।’ ‘अहम्’
बोलकर ही वह दूसरे
शरीर में प्रवेश करता है। जीव का इसी प्रकार आवागमन हुआ करता है। ब्रह्मा
से लेकर सभी जीवों में अहंकार भरा हुआ है जिसमें अहंकार नहीं उसका आवागमन
नहीं होता। ‘अहम’ बोलने से उसका आवागमन सम्बन्ध बराबर
जारी
रहता है। ‘अहम्’ कर्मों का आकर्षण है। यह एक योनि से
खींचकर
दूसरी में डाल देता है।
तीसरा-
क्रियमाण कर्म वह है जो हम अब कर रहे हैं। यदि क्रियमाण कर्म बलवान
होकर शुभ या अशुभ की ओर झुका तो वह अपना रंग-ढंग दिखला देता है। सुकर्म की
ओर झुकने पर यह अपने स्वरूप को दिखा देता है यदि अशुभ की ओर झुका तो जड़
योनि में जा समाता है और नारकीय दुःखों को सहन करता है। फिर उसे सुपथ नहीं
मिल पाता।
कर्म-बन्धन से मुक्त होने की तीन विधियाँ हैं—आप महाभोगी, महात्यागी और महाकर्ता बनकर कर्म-बन्धन से मुक्त हो सकते हैं।
1. महाभोगी उसको कहते हैं जो सब भोग भोगता है किन्तु अपने को भोक्ता नहीं मानता।
2. महात्यागी उसे कहते हैं जो अहंकार को त्याग दे। इस त्याग की परख है—साधक का अन्तर्मुखी होना। अन्तर्मुखी साधक ही महात्यागी बन सकता है।
3. महाकर्ता वह तब होता है जब वह अन्तर्दृष्टि से भली-भाँति देखता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं निरर्थक ही अपने को किसी कार्य का कर्ता समझ रहा हूँ। करने वाला तो कोई और ही है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। जब मैं स्वयं कुछ करता ही नहीं तो अपने को कर्ता क्यों मानूँ ? ऐसी धारणा बनते ही उसका अज्ञान तिरोहित हो जाता है। अज्ञानी जीव अपने को कर्मों का कर्ता मान कर दुख और सुख के धक्के खाता रहता है। हमारे कर्मों के बन्धन ही हमसे ‘अहम्’ बुलवाते हैं। जब हम अपने कर्मों के बन्धन से छूट जायेंगे तब हमारा ‘अहम्’ बोलना भी छूट जाएगा। अकर्ता मानकर जीव अपने शुभ-अशुभ कर्मों को परमेश्वर को सौंप कर उनकी शरण में चला जाता है
जीव कर्मों में स्वतन्त्र नहीं है। यह स्वतन्त्रता केवल सद्गुरु को प्राप्त है। वे जिसको मन से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, दिला देते हैं। जैसा कार्य मनुष्य जाग्रत अवस्था में करता है वैसा ही कार्य स्वप्न अवस्था में करता है किन्तु स्वप्नावस्था के कार्यों को वह अपना कार्य नहीं मानता। जाग्रत स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीया ये व्यक्ति की चार अवस्थायें हैं। जीव के लिए जाग्रत और स्वप्न दोनों अवस्थायें समान हैं केवल यही अन्तर है कि जाग्रत अवस्था देर तक रहती है और स्वप्न थोडी ही देर में बीत जाता है। यदि स्वप्न के कर्म उसके नहीं तो जाग्रत के कर्म भी उसके नहीं हैं। जीव की चारों दशायें स्वप्न के समान हैं।
महाभोगी वह है जो समस्त भोगों को भोगता है और अपने आपको भोगने वाला नहीं मानता। महात्यागी तब होता है जब देह के अभिमान को छोड़े। जब तक देह का अभिमान न छूटे तब तक उसे त्यागी नहीं कहा जा सकता। अभिमान करके ही यह देह मिलती है और इसी अभिमान में स्थित हो रही है। सब त्यागियों में बड़े शुकदेव जी थे जो माया के भय से बारह वर्ष पर्यन्त माता के गर्भ में रहे जब बाहर निकले तब भी उनमें त्याग और वैराग्य बना रहा। सन्त कबीर की शेख तकी ने 52 परीक्षायें लीं अनेक कष्ट दिए पर उन्होंने अन्त में उसे क्षमा कर दिया और कहा—
कर्म-बन्धन से मुक्त होने की तीन विधियाँ हैं—आप महाभोगी, महात्यागी और महाकर्ता बनकर कर्म-बन्धन से मुक्त हो सकते हैं।
1. महाभोगी उसको कहते हैं जो सब भोग भोगता है किन्तु अपने को भोक्ता नहीं मानता।
2. महात्यागी उसे कहते हैं जो अहंकार को त्याग दे। इस त्याग की परख है—साधक का अन्तर्मुखी होना। अन्तर्मुखी साधक ही महात्यागी बन सकता है।
3. महाकर्ता वह तब होता है जब वह अन्तर्दृष्टि से भली-भाँति देखता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं निरर्थक ही अपने को किसी कार्य का कर्ता समझ रहा हूँ। करने वाला तो कोई और ही है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। जब मैं स्वयं कुछ करता ही नहीं तो अपने को कर्ता क्यों मानूँ ? ऐसी धारणा बनते ही उसका अज्ञान तिरोहित हो जाता है। अज्ञानी जीव अपने को कर्मों का कर्ता मान कर दुख और सुख के धक्के खाता रहता है। हमारे कर्मों के बन्धन ही हमसे ‘अहम्’ बुलवाते हैं। जब हम अपने कर्मों के बन्धन से छूट जायेंगे तब हमारा ‘अहम्’ बोलना भी छूट जाएगा। अकर्ता मानकर जीव अपने शुभ-अशुभ कर्मों को परमेश्वर को सौंप कर उनकी शरण में चला जाता है
जीव कर्मों में स्वतन्त्र नहीं है। यह स्वतन्त्रता केवल सद्गुरु को प्राप्त है। वे जिसको मन से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, दिला देते हैं। जैसा कार्य मनुष्य जाग्रत अवस्था में करता है वैसा ही कार्य स्वप्न अवस्था में करता है किन्तु स्वप्नावस्था के कार्यों को वह अपना कार्य नहीं मानता। जाग्रत स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीया ये व्यक्ति की चार अवस्थायें हैं। जीव के लिए जाग्रत और स्वप्न दोनों अवस्थायें समान हैं केवल यही अन्तर है कि जाग्रत अवस्था देर तक रहती है और स्वप्न थोडी ही देर में बीत जाता है। यदि स्वप्न के कर्म उसके नहीं तो जाग्रत के कर्म भी उसके नहीं हैं। जीव की चारों दशायें स्वप्न के समान हैं।
महाभोगी वह है जो समस्त भोगों को भोगता है और अपने आपको भोगने वाला नहीं मानता। महात्यागी तब होता है जब देह के अभिमान को छोड़े। जब तक देह का अभिमान न छूटे तब तक उसे त्यागी नहीं कहा जा सकता। अभिमान करके ही यह देह मिलती है और इसी अभिमान में स्थित हो रही है। सब त्यागियों में बड़े शुकदेव जी थे जो माया के भय से बारह वर्ष पर्यन्त माता के गर्भ में रहे जब बाहर निकले तब भी उनमें त्याग और वैराग्य बना रहा। सन्त कबीर की शेख तकी ने 52 परीक्षायें लीं अनेक कष्ट दिए पर उन्होंने अन्त में उसे क्षमा कर दिया और कहा—
शेख तकी भला तुम कीन्हा।
खरा-खोट पारख कर लीन्हा।
खरा-खोट पारख कर लीन्हा।
महात्याग इसी का नाम है।
मीमांसक और जैन कर्म को ही मुक्ति मार्ग समझते हैं। विधि और निषेध दोनों कर्म महाकाल द्वारा ही निर्मित हैं। ये कर्म वहीं तक पहुँचाने की सामर्थ्य रखते हैं। इन कर्मों द्वारा स्वर्ग, नरक आदि प्राप्त होते हैं। कर्मों का विशाल वन है जिसमें यह जीव भूलकर अपने घर से बाहर हो गया है। वन हिंसक जन्तुओं से भरा हुआ है और सूर्य, चन्द्र तारे आदि कुछ दिखाई नहीं देते। न कोई सड़क है न पगडण्डी, इस कारण इस कर्मों के वन से कोई बाहर नहीं हो सकता। कर्म करता है और फिर-फिर कर्म करने के लिए बारम्बार देह धारण करता है। इसको पता नहीं लगता कि वह कौन है जिससे मेरे कर्म का बन्धन कटे। वह कर्म जिससे इनका बन्धन कटे केवल स्वसम्वेद की शिक्षा है उसी से जीव अपरिचित है।
‘स्वसंवेद बोध’ में सन्त कबीर कहते हैं—
प्रथम जीव पक्के रूप में था। तब दूसरा नहीं था। पक्के तत्व के नाम—1 सत्य, 2 विचार, 3 शील, 4 दया, तथा 5 धीरज।
इन पाँच पक्के तत्त्वों का रूप हंसा (जीव) का था। उसके तीन गुण पक्के थे—
1. सत्य और विचार का गुण—विवेक
2. शील और दया का गुण—गुरु भक्ति, साधु भाव
3. धीरज का गुण—वैराग्य।
ये पक्के तीन गुण थे जिनमें हंसा (जीव) रहा।
सत्य की प्रकृतियाँ—1. निर्णय 2. निर्बन्ध 3. प्रकार 4. थीर 5. क्षमा।
विचार की प्रकृतियाँ—1. अस्ति 2. नास्ति, 3. यथार्थ, 4. शुद्धभाव 5. सत्यता।
दया की प्रकृतियाँ—1. अद्रोह, 2. मित्र जीव 3. सम 4. अभय 5. समदृष्टि।
धीरज की प्रकृतियाँ —1. मिथ्या त्याग 2. सत्य ग्रहण 3. निःसन्देह 4. अहंता नाश 5. अचल।
शील की प्रकृतियाँ—1. क्षुधा निवारण 2. प्रिय वचन 3. शान्ति बुद्धि 4. प्रत्यक्ष पारख 5. सब सुख प्रकट।
पाँचों तत्त्वों की पच्चीस प्रकृतियाँ हैं। इनमें हंसा (जीव) का वास था। पक्के तत्वों की पक्की देह थी तब कुछ अनुमान नहीं था। जब अपनी ऐसी देह देखी और सुन्दरता मानी तब बहुत आनन्द हुआ। उस आनन्द में हंसा मिला तो अपने को भूल गया। गफलत पैदा हुई। इस गफलत में एक झाँईं पड़ी। उस झाँई को सब लोग ब्रह्म सच्चिदानंद कहते हैं। उस आनन्द में जीव बूड़ा तथा तब तत्व प्रकृति पलटी। पक्के से कच्चा रूप हुआ। आपा की खबर न रही। तब पाँच पक्के तत्वों से पाँच कच्चे तत्व हुए—1. धीरज से आकाश, 2. दया से वायु 3. शील से तेज 4. विचार से जल और 5 सत्य से धरती।
पाँच पक्के तत्वों से ये 5 कच्चे तत्त्व हुए। उनके तीन कच्चे गुण हुए—
1. धरती और जल से सतोगुण हुआ,
2. अग्नि और वायु से रजोगुण हुआ, और
3. आकाश से तमोगुण हुआ।
पांच कच्चे तत्वों से 25 प्रकृतियाँ हुईं। यह विकार की देह हुई। इसका नाम मानव हुआ तब अहंकार हुआ कि ‘मैं करता हूँ’ इससे इच्छा हुई। उस इच्छा से नारी का रूप हुआ, उससे भोग किया। फिर वह रूप बिनस गया। नारी गर्भ से तीन रूप पैदा हुये—1. जीव, 2. मन, 3. ज्योति।
मीमांसक और जैन कर्म को ही मुक्ति मार्ग समझते हैं। विधि और निषेध दोनों कर्म महाकाल द्वारा ही निर्मित हैं। ये कर्म वहीं तक पहुँचाने की सामर्थ्य रखते हैं। इन कर्मों द्वारा स्वर्ग, नरक आदि प्राप्त होते हैं। कर्मों का विशाल वन है जिसमें यह जीव भूलकर अपने घर से बाहर हो गया है। वन हिंसक जन्तुओं से भरा हुआ है और सूर्य, चन्द्र तारे आदि कुछ दिखाई नहीं देते। न कोई सड़क है न पगडण्डी, इस कारण इस कर्मों के वन से कोई बाहर नहीं हो सकता। कर्म करता है और फिर-फिर कर्म करने के लिए बारम्बार देह धारण करता है। इसको पता नहीं लगता कि वह कौन है जिससे मेरे कर्म का बन्धन कटे। वह कर्म जिससे इनका बन्धन कटे केवल स्वसम्वेद की शिक्षा है उसी से जीव अपरिचित है।
‘स्वसंवेद बोध’ में सन्त कबीर कहते हैं—
प्रथम जीव पक्के रूप में था। तब दूसरा नहीं था। पक्के तत्व के नाम—1 सत्य, 2 विचार, 3 शील, 4 दया, तथा 5 धीरज।
इन पाँच पक्के तत्त्वों का रूप हंसा (जीव) का था। उसके तीन गुण पक्के थे—
1. सत्य और विचार का गुण—विवेक
2. शील और दया का गुण—गुरु भक्ति, साधु भाव
3. धीरज का गुण—वैराग्य।
ये पक्के तीन गुण थे जिनमें हंसा (जीव) रहा।
सत्य की प्रकृतियाँ—1. निर्णय 2. निर्बन्ध 3. प्रकार 4. थीर 5. क्षमा।
विचार की प्रकृतियाँ—1. अस्ति 2. नास्ति, 3. यथार्थ, 4. शुद्धभाव 5. सत्यता।
दया की प्रकृतियाँ—1. अद्रोह, 2. मित्र जीव 3. सम 4. अभय 5. समदृष्टि।
धीरज की प्रकृतियाँ —1. मिथ्या त्याग 2. सत्य ग्रहण 3. निःसन्देह 4. अहंता नाश 5. अचल।
शील की प्रकृतियाँ—1. क्षुधा निवारण 2. प्रिय वचन 3. शान्ति बुद्धि 4. प्रत्यक्ष पारख 5. सब सुख प्रकट।
पाँचों तत्त्वों की पच्चीस प्रकृतियाँ हैं। इनमें हंसा (जीव) का वास था। पक्के तत्वों की पक्की देह थी तब कुछ अनुमान नहीं था। जब अपनी ऐसी देह देखी और सुन्दरता मानी तब बहुत आनन्द हुआ। उस आनन्द में हंसा मिला तो अपने को भूल गया। गफलत पैदा हुई। इस गफलत में एक झाँईं पड़ी। उस झाँई को सब लोग ब्रह्म सच्चिदानंद कहते हैं। उस आनन्द में जीव बूड़ा तथा तब तत्व प्रकृति पलटी। पक्के से कच्चा रूप हुआ। आपा की खबर न रही। तब पाँच पक्के तत्वों से पाँच कच्चे तत्व हुए—1. धीरज से आकाश, 2. दया से वायु 3. शील से तेज 4. विचार से जल और 5 सत्य से धरती।
पाँच पक्के तत्वों से ये 5 कच्चे तत्त्व हुए। उनके तीन कच्चे गुण हुए—
1. धरती और जल से सतोगुण हुआ,
2. अग्नि और वायु से रजोगुण हुआ, और
3. आकाश से तमोगुण हुआ।
पांच कच्चे तत्वों से 25 प्रकृतियाँ हुईं। यह विकार की देह हुई। इसका नाम मानव हुआ तब अहंकार हुआ कि ‘मैं करता हूँ’ इससे इच्छा हुई। उस इच्छा से नारी का रूप हुआ, उससे भोग किया। फिर वह रूप बिनस गया। नारी गर्भ से तीन रूप पैदा हुये—1. जीव, 2. मन, 3. ज्योति।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book