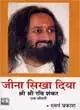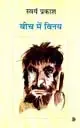|
उपन्यास >> ईंधन ईंधनस्वयं प्रकाश
|
216 पाठक हैं |
|||||||
बचपन की स्मृतियाँ बहुत तृस्त करने वाली हैं। वह तपती रेत पर निरंतर नंगे पैरों की दौड़ जैसा ही है...
Indhan
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
बचपन की स्मृतियाँ बहुत तृस्त करने वाली हैं। वह तपती रेत पर निरंतर नंगे पैरों की दौड़ जैसा ही है। मेरे पिता जी एक प्रेस में कम्पोजीटर थे। गुजारा मुश्किल से ही चलता था। पाँच बहन-भाइयों में मैं सबसे बड़ा था। पिता जी का, लोग कहते थे, किसी दूसरी औरत से सम्बन्ध था। कई रातें उनकी वहीं बीतती थीं। माँ को कोई रहस्यमयी बीमारी थी। पता नहीं पिताजी को भी ठीक से पता था या नहीं कि माँ को क्या बीमारी है। शायद उन्हें पता होगा पर, वह बताते नहीं थे। इतना जरूर है कि बीमारी असाध्य होगी और संक्रामक भी। इसलिए उसका नाम नहीं लिया जाता था।
माँ के सारे बदन में हड्डियाँ निकली हुई थीं। कुछ इस तरह कि वह ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकती थीं। सख्त बिस्तर पर ज़्यादा देर लेटना भी उनके बस का नहीं था। वह दिन रात कराहती रहतीं थीं। एक नौकरानी आकर उनके कपड़े धो जाती थी, कभी-कभी उन्हें नहला भी जाती या उनका बदन गीले तौलिये से पोंछ जाती थी। बाकी घर के कपड़े छोटी बहन धोती थी। सुना यह भी था कि डॉ. गिज़ा के लिए कहते हैं, आबोहवा बदलने के लिए कहते हैं। दोनों चीजें हमारे बस में नहीं थीं। एक बार किसी ने कहा कबूतर का शोरबा पिलाओ, पर यह भी सम्भव नहीं था क्योंकि माँ शाकाहारी थी। वह दवा भी मुश्किल से पीती थीं। उन्होंने अपने तिल-तिल करके मरने को चुपचाप स्वीकार कर लिया था। वह भगवान का नाम भी नहीं लेती थीं। उन्हें किसी चीज की ज़रूरत भी होती तो हमे नहीं पुकारती थीं। पुकारती भी तो उनकी कमज़ोर आवाज़ किसी तरह हम तक नहीं पहुँचती। हम ही बीच-बीच में उनके कमरे मे जाकर पूछ आते-माँ, कुछ चाहिए ?
माँ को देखकर कभी नहीं लगा कि उनके मन में कोई अतृप्त इच्छा अटकी होगी। उन्हें बस दो ही बातों का अफसोस था। एक ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पातीं और दो बच्चों को कुछ बनाकर खिला नहीं पातीं। घर में तो नहीं, पर बाद में अस्पताल में जब हम माँ को देखने या खिचड़ी वगैरह देने जाते-उनकी आँखों में हमें प्यार करने की एक ललक छटपटाती नज़र आती। हम उसे ठीक से समझ नहीं पाते। माँ तब बहुत दिनों तक हमारे दैनिक सुख-दुख से बाहर थीं इसलिए वह हमारे लिए जैसे दूर की कोई रिश्तेदार हो गयी थीं। एक बार उन्होंने अपना हड्डी-हड्डी हाथ मेरे सिर पर फेंरकर पूछा-तू कौन सी क्लास में आ गया ? लेकिन जब मैंने बताया तो मानो उन्होंने सुना ही नहीं।
माँ के सारे बदन में हड्डियाँ निकली हुई थीं। कुछ इस तरह कि वह ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकती थीं। सख्त बिस्तर पर ज़्यादा देर लेटना भी उनके बस का नहीं था। वह दिन रात कराहती रहतीं थीं। एक नौकरानी आकर उनके कपड़े धो जाती थी, कभी-कभी उन्हें नहला भी जाती या उनका बदन गीले तौलिये से पोंछ जाती थी। बाकी घर के कपड़े छोटी बहन धोती थी। सुना यह भी था कि डॉ. गिज़ा के लिए कहते हैं, आबोहवा बदलने के लिए कहते हैं। दोनों चीजें हमारे बस में नहीं थीं। एक बार किसी ने कहा कबूतर का शोरबा पिलाओ, पर यह भी सम्भव नहीं था क्योंकि माँ शाकाहारी थी। वह दवा भी मुश्किल से पीती थीं। उन्होंने अपने तिल-तिल करके मरने को चुपचाप स्वीकार कर लिया था। वह भगवान का नाम भी नहीं लेती थीं। उन्हें किसी चीज की ज़रूरत भी होती तो हमे नहीं पुकारती थीं। पुकारती भी तो उनकी कमज़ोर आवाज़ किसी तरह हम तक नहीं पहुँचती। हम ही बीच-बीच में उनके कमरे मे जाकर पूछ आते-माँ, कुछ चाहिए ?
माँ को देखकर कभी नहीं लगा कि उनके मन में कोई अतृप्त इच्छा अटकी होगी। उन्हें बस दो ही बातों का अफसोस था। एक ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पातीं और दो बच्चों को कुछ बनाकर खिला नहीं पातीं। घर में तो नहीं, पर बाद में अस्पताल में जब हम माँ को देखने या खिचड़ी वगैरह देने जाते-उनकी आँखों में हमें प्यार करने की एक ललक छटपटाती नज़र आती। हम उसे ठीक से समझ नहीं पाते। माँ तब बहुत दिनों तक हमारे दैनिक सुख-दुख से बाहर थीं इसलिए वह हमारे लिए जैसे दूर की कोई रिश्तेदार हो गयी थीं। एक बार उन्होंने अपना हड्डी-हड्डी हाथ मेरे सिर पर फेंरकर पूछा-तू कौन सी क्लास में आ गया ? लेकिन जब मैंने बताया तो मानो उन्होंने सुना ही नहीं।
एक
रोहित
यह बात मैं बहुत दिनों तक नहीं समझ पाया कि स्निग्धा ने मुझसे शादी क्यों की ? अब भी समझ गया हूँ यह कहना ठीक नहीं होगा। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि उसने मुझमें आखिर क्या देखा ? इसमें कोई तर्क नहीं था हमारा कोई जोड़ कोई मुक़ाबला कोई पासंग नहीं था। कोई तुक नहीं थी इसमें। सरासर अविश्वसनीय लगने वाली बात थी। जिन्होंने सुना उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। जो शामिल हुए वे आँखों के सामने सब कुछ होता देखकर भी यकीन करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे थे। और शादी की। शादी के दो साल पहले तक मैं उसे जानता तक नहीं था। वह कहती थी कि वह मुझे जानती थी-हो सकता है देखती जानती रही हो-पर मुझे तो इसमें भी सन्देह है। हम एक ही कॉलेज में थे, लेकिन एक ही कक्षा में नहीं। एक ही फेकल्टी तक में नहीं।
वह आर्ट्स में थी, मैं कॉमर्स में। कॉलेज में बहुत सारे छात्र थे। एक से एक हीरो। मैं तो रात में प्रेस में काम करता था, दिन में ट्यूशनें करता था, खादी का कुरता ज़ीन्स पर लटकाये कॉलेज चला आता था कभी-कभार क्लास भी अटेण्ड कर लेता था। मेरा कॉलेज आना न नियमित था न गंभीर। जाता भी तो एक या डायरी लेकर कैण्टीन में बैठा रहता था। और किताब पढ़ता रहता था या अखबार या डायरी या झोले से प्रूफ निकालकर पढ़ता रहता था और बीड़ियाँ धूँकता रहता था। मुझे डिग्री चाहिए थी जो मैं जानता था कि बगैर नियमित रूप से कक्षा में जाए भी मिल जाएगी। दूसरी तरफ स्निग्धा थी जो कार में बैठकर कॉलेज आती थी और जिसके दीवानों की कोई कमी नहीं थी। दरअसल उसकी अपनी एक टोली थी जिसमें लड़के भी थे, लड़कियाँ भी और जिनका काम उसकी कार में घूमना, पिकनिक मनाना, होटलों में खाना-पीना और जीवन के कुछ वर्ष निश्चिन्त भाव से मटरगश्ती करना था। कुछ और भी रहा हो सकता है। मैं कह नहीं सकता। दरअसल मैं उन लोगों को बहुत कम जानता था-लगभग नहीं के बराबर और जानना जरूरी भी नहीं समझता था। मेरे पास समय ही नहीं था। और होता भी तो उनकी दुनिया मेरी रुचियों के दायरे से बहुत बाहर थी।
शायद स्निग्धा ने अपने किसी आशिक को उसकी बेवफाई या बेरुखी का सबक सिखाने के लिए मुझसे शादी कर ली थी। हो सकता है उसने अपने अकडू बाप से बदला लेने के लिए ही मुझसे शादी कर ली हो। यह भी हो सकता है कि उसने सबके अनुमान ग़लत साबित करने और सबको चौंका देने के लिए ही ऐसा निर्णय ले लिया हो सकता है वह दुनिया को दिखा देना चाहती हो कि वह ज़र्रे को भी आसमान का सितारा बना सकती है। हो सकता है उसके मन में कोई और बात रही हो...लेकिन सच तो यह है कि जब उसने पूछा था-मुझसे शादी करोगे ? तो मैंने यही समझा था कि ये रईस और फैशनेबल छोकरे-छोकरी मिलकर मेरी हँसी उड़ाने की कोई योजना बना बैठे हैं। मैं जानता था कि स्निग्धा पैसा वाली है, बल्कि मैं उसकी कृपा से आक्रांत भी था। एक दिन वह कैण्टीन में मेरी जगह पर बैठी थी और मेरे पहुँचने पर भी उठी नहीं थी, बल्कि उसने मुस्कुराकर मुझसे पूछा था कि कल मैं क्यों नहीं आया ?
वह दिन भर यहीं मेरी प्रतीक्षा करती रही। मुझे ताज्जुब हुआ कि वह मुझे जानती है। मैं क्या कहता ? मैं सकपका गया। मैंने पूछा कुछ काम था ? मेरा प्रश्न उसने सुना ही नहीं...एक कुर्सी खींच लायी....चाय माँग ली...गाल पर हाथ रखकर बैठ गयी और बस देखती रही। मैं चुपचाप चाय पीता रहा और सोचता रहा कि कौन-कौन देख रहा होगा और सोच रहा होगा कि माजरा क्या है ? जब हम चाय पी चुके तो उसने हँसकर कहा कि मैं बीड़ी क्यों नहीं निकाल रहा ?
और खिलखिलायी और फिर मेरी तारीफ करने लगी कि मैं बहुत हेण्डसम हूँ और बहुत मेच्योर हूँ और कुरते में बहुत डेशिंग लगता हूँ और एक अंग्रेज अभिनेता का नाम लिया कि मैं बिल्कुल वैसा लगता हूँ कि जिसका मैंने नाम तक नहीं सुना था और मेरे बाल बहुत दिलफरेब और आवाज़ बहुत दिलकश और आँखें बड़ी मारक हैं और कि मैं बहुत डिफ्रेण्ट हूँ...दूसरों से बहुत अलग हूँ। आदि आदि। इस सबकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मैं अब तक आराम से उसकी सुन्दरता की चपेट में आ चुका था। मैंने आज तक कोई इतनी सुन्दर लड़की इतने पास से नहीं देखी थी। मुझे उसे देखने भर से उसे छूने का एहसास हो रहा था। बल्कि मैं नर्वस हो रहा था। मेरा गला सूख रहा था। मुझे सूझ नहीं रहा था कि उससे क्या बात करूँ ? बल्कि मुझे तो यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ देखूँ ? मुझे डर लग रहा था कि मैं कहीं ऐसी वैसी जगह निगाहें न गड़ा लूँ जोकि बड़ी शर्म की बात हो जाए मेरे लिए। उसके साथ का हर पल एक अलौकिक अभूतपूर्व लेकिन अत्यंत पीड़ादायक आनन्द की वर्षा कर रहा था। मैं असुविधा महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि कब यह स्वर्गिक मुलाक़ात खत्म हो। वह सामने थी और मैं मानसिक रूप से उन क्षणों में पहुँच भी चुका था कि जब वह मुझसे निराश होकर जा चुकी है और मैं अपने चुग़दपने को कोसता, हाथ मलता बैठा रहा गया हूँ।
लेकिन वह समझ रही थी। उसे मालूम था कि ऐसा ही होगा। उसे बुलवाना आता था। उसने एकदम मामूली लगनेवाली बातें करके आधे घण्टे के भीतर ही मुझे खोल लिया और मैं गौरवान्वित सा महसूस करने लगा। हीरो जैसा महसूस करने लगा। सोचने लगा कि सब मुझसे जल रहे हैं। बेशक, बिल भी उसी ने चुकाया और कुल मिलाकर एक ही मुलाकात में उसने मुझे इतना फचीट लिया कि मैं कम से कम एक महीने उसके लिए विह्वल रहूँ।
फिर वह जो मेरे कुरते-ज़ीन्स की तारीफ करती नहीं अघा रही थी, दूसरे दिन दो दो रेडीमेड कमीजें लिये मेरे घर आ धमकी और मेरी सख्त निगरानी के बावजूद उसकी आँखों में मेरे पसमांदा घर के लिए कोई टिप्पणी नहीं पायी जा सकी। जैसे घर के उसे क्या मतलब ? या जैसे घर मेरा नहीं, किसी और का हो। और फिर वह जो मेरे बीड़ी पीने पर मर मिट रही थी-रोज मेरे कुरते की जेब में डालने के लिए एक महँगी सिगरेट का पैकेट लाने लगी। और मैं जन्मजात भुक्खड़ अच्छे होटल की चाय और सिनेमा के बालकनी के टिकट और कार की सवारी और आइसक्रीम और महँगे तोहफों के लालच में लार टपकाता-यह जानते हुए भी कि संभवत मुझसे खेल किया जा रहा है-इस खेल में शामिल हो गया।
इसलिए जब उसने मुझसे कहा-मुझसे शादी करोगे ? तो मैंने यही समझा कि मजाक अब पराकाष्ठा पर पहुँच गया है-अब बस पैसेवाले छोकरे-छोकरियों का सम्मिलित ठहाका गूँजना बाकी है। जब उसने विश्वास दिलाना चाहा कि वह गंभीरतापूर्वक कह रही है तो मैंने गंभीर मुखमुद्रा बनाकर सोचने के लिए महीने भर की मोहलत माँगी-कि अगर इसे रोमांस का बुखार वाकई चढ़ गया है तो महीने भर में तो उतर ही जाएगा। लेकिन उसने इसे मेरी स्वीकृति और अपनी विजय समझा और दूसरे दिन से मेरे लिए टिफ़िन में खाना लेकर रोज़ घर आनेलगी। मैं जितनी देर में खाना खाता, वह घर साफ़ करने जैसा कुछ करती रहती और गुनगुनाती रहती-मानो अभी से मेरे साथ पत्नीवत जीने के पूर्वाभ्यास का मज़ा लेने की कोशिश कर रही हो।
अब वह निरंतर मुझे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करने लगी कि बावजूद सब कुछ के वह भीतर से बेहद दुखी और अकेली लड़की है...कि उसका बाप जालिम है...कि उसके दोस्त खुदगर्ज़ और मतलबी हैं...कि उसके समाज के लोग छिछले और चालू हैं।...कि उसका बचपन नाना प्रकार की अप्रिय बन्दिशों में बीता है...कि उसके दिल की प्यार की प्यास को आज तक किसी ने नहीं समझा है..कि उससे ज़्यादा बदकिस्मत और मनहूस लड़की दुनिया में शायद ही कोई हो वगैरह।
पन्द्रहवें दिन बड़े रहस्यमयी तरीके से मुझे एक कम्पनी में जूनियर अकाउण्ट्स ऑफिसर का इण्टरव्यू कॉल मिला और बगैर किसी धकमपेल उतने ही रहस्यमयी तरीके से मेरा चयन हो गया और मैं जो रातपाली में प्रेस में काम कर रहा था, दिन में टूयूशनें पढ़ा रहा था, बाक़ी बचे समय में प्रूफ पढ़ रहा था, बाकी बचे समय में खुद भी पढ़ रहा था और बाकी बचे समय में रोमांस कर रहा था और बाकी बचे समय में अपनी आज की ज़िन्दगी को ही जैसे सिनेमा के परदे पर चलता देख रहा था...महीने भर बाद एक दिन अचानक अपहृत करके पास के एक शहर में ले जाया गया और बगैर ज़्यादा ढोल-ढमाके के पति बना दिया गया।
लेकिन यहीं से कहानी का करुण मोड़ आरम्भ हो गया। शादी होते ही स्निग्धा को लग गया कि उसने ग़लत निर्णय ले लिया है। जैसे मुँह से ग़लत बात निकलते ही हमें लग जाता है कि ग़लत बात निकल गयी, लेकिन उसे वापस लेने का कोई उपाय शेष नहीं रहता, फिर तो सिर्फ़ उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार होना होता है, उसे लग गया कि हँसी-हँसी में भयंकर भूल हो गयी है। शादी के दौरान ही उसका मुँह लटक गया, आँखों में चमक की जगह चिन्ता आ बैठी, चेहरे की थिरक और पुलक ग़ायब हो गयी...उसके व्यक्तित्व में जो कुछ भी मोहक और मादक था...देखते ही देखते कपूर की तरह उड़ गया और वहाँ एक निरीह-मजबूर ठगी-घिरी-जीव थी थी....अनजान जगह में जिसकी आख़िरी बस चूक गयी हो...या बीच धार जिसकी नाव में बड़ा सा सुराख हो गया हो या हाथ से चप्पू छूटकर लहरों में बह गया हो....या मेले में जिसकी जेब कट गयी हो...या ऑपरेशन के दौरान जिसकी नाक से ऑक्सीजन की नली निकल गयी हो।
शायद बदला लेने या दुनिया को दिखा देने के रास्ते यहाँ से आगे कहीं नहीं जाते थे। आगे एक नीरस ज़िन्दगी और रुटीन गृहस्थी थी जो सारी निजता और स्वतंत्रता का एक झटके से हरण कर लेती थी और वरण के सारे विकल्पों का एक साथ समापन कर देती थी। अब आगे चुनने को कुछ नहीं था। अब आगे सिर्फ़ एक अस्पष्ट पगडंडी जो अनिश्चय और आशंका की धुंध में डूबी हुई थी....जिस पर चलना पता नहीं कहाँ ले जा सकता था लेकिन जिससे वापसी के सारे पुल वह स्वयं अभी-अभी अपने हाथों जला चुकी थी।
मैं शादी के लिए तैयार हो गया था-यह कहना भी ग़लत ही होगा। हाँ, मेरा मन शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करने का बन रहा था, यह ज़रूर है। क्योंकि मन ही मन मुझे लालच था कि बड़े घर के साथ रिश्ता जुड़ने से मुझे तरह-तरह के लाभ हो सकते हैं-घाटा तो कोई भी नहीं है और दूसरे, वैसे भी मुझसे शादी कौन करता ?
इस तरह बग़ैर पूरी मानसिक तैयारी के हम पति-पत्नी हो गये।
बचपन की स्मृतियाँ बहुत त्रस्त करने वाली हैं। वह तपती रेतपर निरंतर चलती नंगे पैरों की दौड़ जैसा ही है। मेरे पिताजी एक प्रेस में कम्पोज़ीटर थे। गुजारा मुश्किल से ही चलता था। पाँच बहन-भाइयों में मैं सबसे बड़ा था। पिताजी का, लोग कहते थे, किसी दूसरी औरत से सम्बन्ध था। कई रातें उनकी वहीं बीतती थीं। माँ को कोई रहस्यमयी बीमारी थी। पता नहीं पिताजी को भी ठीक से पता था या नहीं कि माँ को क्या बीमारी है। शायद उन्हें पता होगा, पर वह बताते नहीं थे। इतना ज़रूर है कि बीमारी असाध्य होगी और संक्रामक भी। इसीलिए उसका नाम नहीं लिया जाता था। माँ के सारे बदन में हड्डियाँ निकली हुई थीं। कुछ इस तरह कि वह ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकती थीं। सख़्त बिस्तर पर ज़्यादा देर लेटना भी उनके बस का नहीं था। वह दिन रात कराहती रहती थीं। एक नौकरानी आकर उनके कपड़े धो जाती थी, कभी-कभी उन्हें नहला भी जाती थी या उनका बदन गीले तौलिये से पोंछ जाती थी। बाकी घर के कपड़े छोटी बहन धोती थी। सुना यह भी था कि डॉक्टर गिज़ा के लिए कहते हैं, आबोहवा बदलने के लिए कहते हैं
।
दोनों चीज़े हमारे बस में नहीं थीं। एक बार किसी ने कहा कि कबूतर का शोरबा पिलाओ, पर यह भी संभव नहीं था, क्योंकि माँ शाकाहारी थीं। वह दवा भी मुश्किल से ही पीती थीं। उन्होंने अपने तिल-तिल करके मरने को चुपचाप स्वीकार कर लिया था। वह भगवान का नाम भी नहीं लेती थीं। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत भी होती तो हमें नहीं पुकारतीं। पुकारतीं भी तो उनकी कमज़ोर आवाज़ किसी तरह हम तक नहीं पहुँचती। हम ही बीच-बीच में उनके कमरे में जाकर पूछ आते-माँ, कुछ चाहिए ?
माँ को देखकर कभी नहीं लगा कि उनके मन में कोई अतृप्त इच्छा अटकी होगी। उन्हें बस दो ही बातों का अफसोस था। एक-ठाकुरजी सेवा नहीं कर पातीं और दो बच्चों को कुछ बनाकर खिला नहीं पातीं। घर में तो नहीं, पर बाद में अस्पताल में जब हम माँ को देखने या खिचड़ी वगैरह देने जाते-उनकी आँखों में हमें प्यार करने की एक गहरी ललक छटपटाती नज़र आती। हम उसे ठीक से समझ नहीं पाते। माँ तब बहुत दिनों से हमारे दैनिक सुख-दुख से बाहर थीं इसलिए वह हमारे लिए जैसे दूर की कोई रिश्तेदार हो गयी थीं। एक बार उन्होंने अपना हड्डी-हड्डी हाथ मेरे सिर पर फेरकर पूछा-तू कौन सी क्लास में आ गया ? लेकिन जब मैंने बताया तो मानो उन्होंने सुना ही नहीं।
माँ कोई बहुत अच्छी कुक नहीं थीं। बीमारी की वजह से हमें कुछ बनाकर खिलाने का अवसर उन्हें कम ही मिलता था। फिर भी कभी-कभी खासकर, वार-त्यौहार वह अपनी सारी ताकत लगाकर उठतीं और रसोई में आ जातीं। लेकिन रसोई उनकी पसन्द की नहीं होती ! वहाँ कुछ भी अच्छा पकाने के वातावरण का अभाव रहता। या तो मसालदान खाली होता या आटे के पीपे का पेंदा दिखाई दे रहा होता या जूठे बरतन भिनक रहे होते या स्टोव में केरोसीन इतना कम होता कि वह बार-बार भभक या बुझ रहा होता। सफाई तो नहीं ही होती। हम बहन-भाइयों द्वारा की गयी टालमटोल सफ़ाई माँ के लिए गन्दगी लीप देने का ही पर्याय होती। कभी जब सारी चीजें अनुकूल होतीं तो माँ की हँफनी और चक्कर और बाँयठे और अँधेरी उन्हें ज़्यादा देर बैठने नहीं देती। अनुष्ठान की तरह आरम्भ किया पाकप्रयास उन्हें बीच राह बेटी के हवाले कर फिर अपनी खटिया की शरण लेनी पड़ती। फिर भी कभी-कभी वह बड़ी कड़ाही में आटे का घोल उबलवातीं और उसमें ढेर सारा गुड़ का पानी मिलाकर एक तरह की मीठी लेई बनवा देतीं। कहना न होगा कि हम लोग न सिर्फ़ उसे खुश होकर खाते, बल्कि देर तक चाट-चाटकर खाते और उसके लिए लड़ते भी। हम उसे खाना भी चाहते और यह भी नहीं चाहते कि वह खत्म हो जाए। दूसरे दिन भी उसी की बात करते।
घर में मेहमान आये एक अर्सा हुआ था। लेकिन बड़े-बच्चों जैसे मैं और मेरी बहन के मन में मेहमान आने की स्मृति सुरक्षित थी। मेहमानों की स्मृति का सीधा संबंध खाने से था। उन्हें अच्छा खाना खिलाया ही जाता था। वह कुछ-कुछ मात्रा में हमें भी मिल जाता था। कोई-कोई मेहमान अपने साथ किसी एक को घुमाने भी ले जाते थे-लोकल गाइड की बतौर। तब आइसक्रीम, चाट या सोडावाटर का मिलना निश्चित था। घर से निकलने से पहले ही इन क्षणों की प्रतीक्षा शुरू हो जाती थी। जब वे लोग कुछ खाएँगे-पिएँगे और हमें भी मिलेगा। घर लौटकर उत्सुक भाई-बहनों को बताते कि क्या-क्या मिला। कभी-कभी तो हम खुद मेहमानों को बताते चलते कि अमुक दुकान की आइसक्रीम बहुत प्रसिद्ध है और फलाँ ठेलेवाले की चाट बाहर से जो आता है, एक बार ज़रूर खाता है।
इसलिए हमारे दोस्त भी वही थे जो बीच की छुट्टी में हमें अमरूद, ककड़ी, नमकीन वगैरह खिला सकें, या जिनके घर जाओ तो कुछ न कुछ खाने को मिले। बल्कि हम उनके दोस्त क्या, चमचे थे। मैं तो था ही। मैं हर लड़ाई में उनका पक्ष लेता, दौड़-दौड़कर उनका काम करता, उनका होमवर्क कर देता और उनका बैग, उनके जूते तक उठाकर चलता। वे जानते थे। वे करवाते। उन्हें मज़ा आता। मुझे झेंप लगती। फिर भी करता। दोस्तों के घर रोज़-रोज़ खाने पीने में शर्म लगती, क्योंकि जवाब में उन्हें कभी अपने घर बुलाकर कुछ नहीं खिला सकता था-फिर भी रोज़ जाता और जानबूझ कर ऐसे टाईम जब उनका खाने, नाश्ते या दोपहरी का वक़्त हो, एक बार एक दोस्त की मम्मी ने पूछ भी लिया-क्यों रे ? तेरी मइया तुझे कुछ नहीं खिलाती ? भूखा रखती है ? दिनेश के हिस्से का खाने आ जाता है ? सुनकर कान जलने लगे। बाहर आकर अपने ही हाथों से अपने गालों पर दो झापड़ मारे और सारे रास्ते खूब रोया। दूसरे दिन दिनेश ने माफी भी माँगी, पर फिर उसके घर कभी नहीं गया।
सब्ज़ी ख़रीदकर लाने के लिए हम दोनों भाई तैयार रहते थे। सब्ज़ी लाने मण्डी जाना पड़ता था। पैदल। तीन किलोमीटर। लौटते समय दो बड़े और भरे थैले दोनों हाथों में उठाकर लाने पड़ते थे। हाथ दुख जाते थे। सो भी शाम के वक्त। जब मालनें उठनेवाली हों और सारी बची खुची सब्ज़ी सस्ते दाम खाली कर घर जाने के मूड में हों। यानी उस दिन अपने खेल का भी बलिदान। लेकिन सब्ज़ी में से आराम से दस पैसे मारे जा सकते थे। दस पैसे में तीन गोलगप्पे आते थे, या दो नानखटाई या चार लेमनचूस या आठ मीठी गोली या एक चूरन की पुड़िया। गोलगप्पेवाला नखरे लगाता। सारी भीड़ को निबटाकर फिर ध्यान देता। पैसे पहले माँगता। हाथ में लेकर उलट-पटल कर देखता कि खोटा तो नहीं है। फिर गोलगप्पे देता-जिन्हें जल्दी-जल्दी खा लेना पड़ता कि कोई जान पहचानवाला देख न ले-फिर और खाली पानी माँगते, दो बार-वह उसमें भी नखरे लगाता। लेकिन रोज़-रोज़ बेस्वाद फीकी खिचड़ी या सूखी रोटी निगलनेवाली ज़बान को तो इतने से स्वाद से भी मजा आ जाता।
कुछ बड़ा हुआ तो चोरी शुरू कर दी। तरकीब आसान थी। बड़े लड़कों के साथ अँधेरा होने तक फुटबॉल खेलते। खेल ख़त्म हो जाने पर मैदान पर कहीं भी घेरा बनाकर बैठ जाते और गपशप करते। मैदान के साथ-साथ चलती सड़क से बैलगाड़ियाँ गुजरतीं। बड़े लड़के मौक़ा ताड़कर किसी भी बैलगाड़ी के पीछे लग जाते और पीछे से चढ़कर जो जितना हाथ में आये, भर-उठा लाते। कभी गन्ना, कभी फूलगोभी कभी गुड़ की भेली, कभी मूली, कभी मूँगफली। मूँगफली सब बाँटकर खाते। कुछ रोज बाद मुझसे कहा गया। ललकारा गया। मैं गया दबे पाँव। चलती गाड़ी पर चढ़ भी गया, गुड़ था, उठा भी लिया, पर जाने कैसे गाड़ीवाले को पता चल गया। वह चलती गाड़ी से कूद पीछे की तरफ आया। दोस्तों की आवाजें आयीं-साले भाग ! पर मैं कूदने में देर कर गया। गाड़ी चल रही थी। मैं डर गया कि सम्हलकर नहीं कूदा तो गिर जाऊँगा। और सम्हलकर कूदा-कूदा कि गाड़ीवाले ने अपने मजबूत हाथ में मेरी कलाई भींच ली और ज़ोर का झापड़ मारा। मैं बिलबिलाकर रोया, मैंने हाथ की भेली नीचे फेंक दी, मुझे पुलिस में दिये जाने का डर लगा और मेरी निकर में पेशाब निकल आया। मेरी दशा देखकर गाड़ीवाले को हँसी आ गयी और उसने मुझे सिर पर टप्पल मारकर छोड़ दिया। उस दिन सारे दोस्त मुझ पर खूब हँसे। लेकिन धीरे-धीरे एकस्पर्ट हो गया।
मैं भुक्खड़ ! जन्मजात भुक्खड़ ! घर में कोई चीज़ बनवाकर खाता हूँ तो भुक्खड़। कुछ बनाने की फरमाइश करता हूँ तो भुक्खड़। कोई चीज़ अच्छी लगती है और चट कर जाता हूँ तो भुक्खड़ ! बीवी का ख़याल है खा पीकर प्लेट को चाटना या प्लेट को उँगली से पोंछकर उँगली को चाटना भुक्खड़पन होता है। उसका ख़याल है कि प्लेट में जरूर कुछ न कुछ छोड़ना चाहिए। मसलन भजिये बने हों तो चार भजिये खाकर मुझे आप लीजिए, आप लीजिए, करने लगना चाहिए। मुझे मेरे बेटे के आगे एक गन्दी मिसाल की तरह पेश किया जाता है। ‘‘खाओ, ज़रा तमीज़ से अपने पापा की तरह नहीं।’
माँ की बीमारी इस ख़याल से छिपायी जा रही थी कि मोहल्लेवाले या स्कूल के बच्चे हमसे ही छूत न बरतने लगें। लेकिन सारे मोहल्ले को पता था कि माँ मर रही हैं। इसलिए जब वह एक दिन सचमुच मर गयीं तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। धक्का नहीं लगा। खुद हमें भी नहीं। पिताजी ज़रूर रोये। फूट-फूटकर लेकिन उनका रोना देखकर उन पर दया नहीं आ रही थी-गुस्सा आ रहा था। उन्हें एक थप्पड़ रसीद करने की इच्छा हो रही थी।
माँ के मरने के दो महीने बाद एक दिन अचानक पिताजी गायब हो गये। कोई कहता था वह साधु हो गये, कोई कहता था दूसरी औरत के साथ भाग गये। एक पूरे सप्ताह हम पाँचों भाई-बहन उनकी प्रतीक्षा करते रहे और रोते रहे और पड़ोसियों के यहाँ से आयी रोटियाँ खाते रहे और तरह-तरह की योजनाएँ बनाते रहे। मैं भाई-बहनों को समझाता रहा कि हम कोई भी काम कर लेंगे, मेहनत मजदूरी कुछ भी और गुज़ारा चला लेंगे किसी तरह लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगे।
वे अविश्वास से मुझे अपलक देखते और फिर रोने लगते। आठवें रोज़ गाँव से मामाजी आ गये और हम सबको अपने साथ गाँव ले गये। घी दूध का प्रचुरता का लालच देकर। उस साल मुझे दसवीं की परीक्षा देनी थी। गाँव में हम सबके लिए सुबह से रात तक हाड़तोड़ काम था। पढ़ाई का सवाल ही नहीं था। फिर भी छोटे बहन-भाई वहीं रहना चाहते थे। एक दिन मैं वहाँ से भागकर वापस शहर आ गया और उसी प्रेस के आगे जाकर खड़ा हो गया भूखा प्यासा जिसमें पिताजी काम करते थे।
दया करके मुझे रख लिया गया। सुबह-सुबह मैं झाड़ू लगा देता, पानी भर देता, साफ-सफाई कर डालता, चाय-पानी ले आता, चेसिस धो देता, गैली प्रूफ उठा लेता और समय मिलते ही डिस्ट्रीब्यूट करने बैठ जाता। प्रेस के एक पुराने कर्मचारी सीतारामजी टिफिन में मेरे लिए भी दो रोटियाँ डलवाकर घर से ले आते और लंच टाइम में बड़े प्यार से मुझे पकड़ा देते। मैं खा लेता। रात को वहीं जमीन पर चादर बिछाकर सो जाता।
दिमाग तेज़ था। फटाफट काम सीख गया। भाषा अच्छी थी। हिन्दी अंग्रेजी के प्रूफ भी पढ़ देता। एक बार कोई किताब पढ़ लेता तो याद हो जाती। उस साल दसवीं में प्रथम श्रेणी से पास हुआ। प्रेस में ही एक दिन पाटोदिया साहब से मुलाकात हुई। वह चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट थे। कुछ छपाने आये थे। उनके ड्राफ्ट में मैंने एक गलती निकाल दी। हुज्जत करने लगा। डिक्शनरी मँगायी गयी। मैं सही निकला। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा। प्रेममालिक से मेरे बारे में पूछताछ की। चले गये। अगले दिन फिर आये। प्रेसमालिक के पास बैठे। वहाँ मुझे बुलवाया गया। पूछा गया कि क्या मैं पाटोदिया साहब के बच्चों को एक घण्टा पढ़ा दूँगा ?
पाटोदिया साहब का बहुत बड़ा मकान था और बहुत जमी हुई प्रेक्टिस। सम्पन्न व्यक्ति थे। तीन बच्चियाँ थीं। पत्नी शांत हो गयी थीं। माँ घर सम्हालती थीं। वहाँ मुझे अच्छा लगा। बच्चे मुझसे हिल गये। पाटोदिया साहब प्रभावित। प्यार करने की हद तक। मुझे नीचेवाला कमरा दे दिया गया। खाना भी वहीं खाने लगा। कुछ रोज़ बाद दफ्तर के काम में भी उनकी मदद करने लगा। वह कहते थे आदमी मेहनत से जी न चुराये और लगन से काम करे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। हायर सेकंडरी में फर्स्ट डिवीज़न आया। होशियार बच्चे साइंस लेते थे। मैंने कॉमर्स ली। मुझे पाटोदिया साहब जैसा बनना था। लेकिन कमरा बदल लिया। प्रेस की नौकरी छोड़ी नहीं।
बहुत दिन बाद एक दिन अचानक एक दूध की दूकान पर छोटा भाई दिखाई दे गया। आँखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। लिपट गये। वहीं बैठकर बातें करने लगे। भाई ने बताया दो बहनों की शादी हो चुकी है, तीसरी पाँव रपट जाने से कुएँ में गिर गयी और मर गयी। फिर वह मुझसे गाँव चलने की ज़िद करने लगा और मैं उससे अपने घर चलने की। मैं आहत था और उफन रहा था कि मेरी सगी छोटी बहनों के विवाह की मुझे सूचना तक नहीं दी गयी-बगैर यह सोचे कि सूचना कहाँ किस पते पर दी जाती ? भाई घर नहीं आया, मैं गाँव नहीं गया। दोनों पलटकर अपने-अपने रास्ते चले गये।
इसके बाद उसे नहीं देखा।
स्निग्धा ने सोचा था उसकी शादी से शहर भर में हंगामा हो जाएगा। घर में तूफान मच जाएगा और कॉलेज में जिसे पता चलेगा उसका मुँह खुला का खुला रह जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। फिर विश्वास हुआ तो स्निग्धा की बेवकूफी पर तरस आया और लोगों ने उसे मुबारकबाद भी ऐसे दी जैसे सांत्वना दे रहे हों। और तो और किसी ने पार्टी भी नहीं माँगी। इससे वह और दुखी हो गयी और अपने आप पर और ज़्यादा झुँझलाने लगी। इससे उसकी कम हो चुकी सुन्दरता और कम हो गयी। उसने सोचा उसके ग्रुप में न सही उसकी अंतरंग सहेलियों में से तो कोई होगी ही जो उसे इस साहसिक निर्णय की प्रशंसा करेगी, लेकिन यहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगी। अंतरंग सहेलियों की प्रतिक्रिया और ज़्यादा छीलने वाली थी। कम से कम बताना तो था। इतना बड़ा स्टेप ले लिया और एक बार बताया तक नहीं।
यह बात मैं बहुत दिनों तक नहीं समझ पाया कि स्निग्धा ने मुझसे शादी क्यों की ? अब भी समझ गया हूँ यह कहना ठीक नहीं होगा। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि उसने मुझमें आखिर क्या देखा ? इसमें कोई तर्क नहीं था हमारा कोई जोड़ कोई मुक़ाबला कोई पासंग नहीं था। कोई तुक नहीं थी इसमें। सरासर अविश्वसनीय लगने वाली बात थी। जिन्होंने सुना उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। जो शामिल हुए वे आँखों के सामने सब कुछ होता देखकर भी यकीन करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे थे। और शादी की। शादी के दो साल पहले तक मैं उसे जानता तक नहीं था। वह कहती थी कि वह मुझे जानती थी-हो सकता है देखती जानती रही हो-पर मुझे तो इसमें भी सन्देह है। हम एक ही कॉलेज में थे, लेकिन एक ही कक्षा में नहीं। एक ही फेकल्टी तक में नहीं।
वह आर्ट्स में थी, मैं कॉमर्स में। कॉलेज में बहुत सारे छात्र थे। एक से एक हीरो। मैं तो रात में प्रेस में काम करता था, दिन में ट्यूशनें करता था, खादी का कुरता ज़ीन्स पर लटकाये कॉलेज चला आता था कभी-कभार क्लास भी अटेण्ड कर लेता था। मेरा कॉलेज आना न नियमित था न गंभीर। जाता भी तो एक या डायरी लेकर कैण्टीन में बैठा रहता था। और किताब पढ़ता रहता था या अखबार या डायरी या झोले से प्रूफ निकालकर पढ़ता रहता था और बीड़ियाँ धूँकता रहता था। मुझे डिग्री चाहिए थी जो मैं जानता था कि बगैर नियमित रूप से कक्षा में जाए भी मिल जाएगी। दूसरी तरफ स्निग्धा थी जो कार में बैठकर कॉलेज आती थी और जिसके दीवानों की कोई कमी नहीं थी। दरअसल उसकी अपनी एक टोली थी जिसमें लड़के भी थे, लड़कियाँ भी और जिनका काम उसकी कार में घूमना, पिकनिक मनाना, होटलों में खाना-पीना और जीवन के कुछ वर्ष निश्चिन्त भाव से मटरगश्ती करना था। कुछ और भी रहा हो सकता है। मैं कह नहीं सकता। दरअसल मैं उन लोगों को बहुत कम जानता था-लगभग नहीं के बराबर और जानना जरूरी भी नहीं समझता था। मेरे पास समय ही नहीं था। और होता भी तो उनकी दुनिया मेरी रुचियों के दायरे से बहुत बाहर थी।
शायद स्निग्धा ने अपने किसी आशिक को उसकी बेवफाई या बेरुखी का सबक सिखाने के लिए मुझसे शादी कर ली थी। हो सकता है उसने अपने अकडू बाप से बदला लेने के लिए ही मुझसे शादी कर ली हो। यह भी हो सकता है कि उसने सबके अनुमान ग़लत साबित करने और सबको चौंका देने के लिए ही ऐसा निर्णय ले लिया हो सकता है वह दुनिया को दिखा देना चाहती हो कि वह ज़र्रे को भी आसमान का सितारा बना सकती है। हो सकता है उसके मन में कोई और बात रही हो...लेकिन सच तो यह है कि जब उसने पूछा था-मुझसे शादी करोगे ? तो मैंने यही समझा था कि ये रईस और फैशनेबल छोकरे-छोकरी मिलकर मेरी हँसी उड़ाने की कोई योजना बना बैठे हैं। मैं जानता था कि स्निग्धा पैसा वाली है, बल्कि मैं उसकी कृपा से आक्रांत भी था। एक दिन वह कैण्टीन में मेरी जगह पर बैठी थी और मेरे पहुँचने पर भी उठी नहीं थी, बल्कि उसने मुस्कुराकर मुझसे पूछा था कि कल मैं क्यों नहीं आया ?
वह दिन भर यहीं मेरी प्रतीक्षा करती रही। मुझे ताज्जुब हुआ कि वह मुझे जानती है। मैं क्या कहता ? मैं सकपका गया। मैंने पूछा कुछ काम था ? मेरा प्रश्न उसने सुना ही नहीं...एक कुर्सी खींच लायी....चाय माँग ली...गाल पर हाथ रखकर बैठ गयी और बस देखती रही। मैं चुपचाप चाय पीता रहा और सोचता रहा कि कौन-कौन देख रहा होगा और सोच रहा होगा कि माजरा क्या है ? जब हम चाय पी चुके तो उसने हँसकर कहा कि मैं बीड़ी क्यों नहीं निकाल रहा ?
और खिलखिलायी और फिर मेरी तारीफ करने लगी कि मैं बहुत हेण्डसम हूँ और बहुत मेच्योर हूँ और कुरते में बहुत डेशिंग लगता हूँ और एक अंग्रेज अभिनेता का नाम लिया कि मैं बिल्कुल वैसा लगता हूँ कि जिसका मैंने नाम तक नहीं सुना था और मेरे बाल बहुत दिलफरेब और आवाज़ बहुत दिलकश और आँखें बड़ी मारक हैं और कि मैं बहुत डिफ्रेण्ट हूँ...दूसरों से बहुत अलग हूँ। आदि आदि। इस सबकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मैं अब तक आराम से उसकी सुन्दरता की चपेट में आ चुका था। मैंने आज तक कोई इतनी सुन्दर लड़की इतने पास से नहीं देखी थी। मुझे उसे देखने भर से उसे छूने का एहसास हो रहा था। बल्कि मैं नर्वस हो रहा था। मेरा गला सूख रहा था। मुझे सूझ नहीं रहा था कि उससे क्या बात करूँ ? बल्कि मुझे तो यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ देखूँ ? मुझे डर लग रहा था कि मैं कहीं ऐसी वैसी जगह निगाहें न गड़ा लूँ जोकि बड़ी शर्म की बात हो जाए मेरे लिए। उसके साथ का हर पल एक अलौकिक अभूतपूर्व लेकिन अत्यंत पीड़ादायक आनन्द की वर्षा कर रहा था। मैं असुविधा महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि कब यह स्वर्गिक मुलाक़ात खत्म हो। वह सामने थी और मैं मानसिक रूप से उन क्षणों में पहुँच भी चुका था कि जब वह मुझसे निराश होकर जा चुकी है और मैं अपने चुग़दपने को कोसता, हाथ मलता बैठा रहा गया हूँ।
लेकिन वह समझ रही थी। उसे मालूम था कि ऐसा ही होगा। उसे बुलवाना आता था। उसने एकदम मामूली लगनेवाली बातें करके आधे घण्टे के भीतर ही मुझे खोल लिया और मैं गौरवान्वित सा महसूस करने लगा। हीरो जैसा महसूस करने लगा। सोचने लगा कि सब मुझसे जल रहे हैं। बेशक, बिल भी उसी ने चुकाया और कुल मिलाकर एक ही मुलाकात में उसने मुझे इतना फचीट लिया कि मैं कम से कम एक महीने उसके लिए विह्वल रहूँ।
फिर वह जो मेरे कुरते-ज़ीन्स की तारीफ करती नहीं अघा रही थी, दूसरे दिन दो दो रेडीमेड कमीजें लिये मेरे घर आ धमकी और मेरी सख्त निगरानी के बावजूद उसकी आँखों में मेरे पसमांदा घर के लिए कोई टिप्पणी नहीं पायी जा सकी। जैसे घर के उसे क्या मतलब ? या जैसे घर मेरा नहीं, किसी और का हो। और फिर वह जो मेरे बीड़ी पीने पर मर मिट रही थी-रोज मेरे कुरते की जेब में डालने के लिए एक महँगी सिगरेट का पैकेट लाने लगी। और मैं जन्मजात भुक्खड़ अच्छे होटल की चाय और सिनेमा के बालकनी के टिकट और कार की सवारी और आइसक्रीम और महँगे तोहफों के लालच में लार टपकाता-यह जानते हुए भी कि संभवत मुझसे खेल किया जा रहा है-इस खेल में शामिल हो गया।
इसलिए जब उसने मुझसे कहा-मुझसे शादी करोगे ? तो मैंने यही समझा कि मजाक अब पराकाष्ठा पर पहुँच गया है-अब बस पैसेवाले छोकरे-छोकरियों का सम्मिलित ठहाका गूँजना बाकी है। जब उसने विश्वास दिलाना चाहा कि वह गंभीरतापूर्वक कह रही है तो मैंने गंभीर मुखमुद्रा बनाकर सोचने के लिए महीने भर की मोहलत माँगी-कि अगर इसे रोमांस का बुखार वाकई चढ़ गया है तो महीने भर में तो उतर ही जाएगा। लेकिन उसने इसे मेरी स्वीकृति और अपनी विजय समझा और दूसरे दिन से मेरे लिए टिफ़िन में खाना लेकर रोज़ घर आनेलगी। मैं जितनी देर में खाना खाता, वह घर साफ़ करने जैसा कुछ करती रहती और गुनगुनाती रहती-मानो अभी से मेरे साथ पत्नीवत जीने के पूर्वाभ्यास का मज़ा लेने की कोशिश कर रही हो।
अब वह निरंतर मुझे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करने लगी कि बावजूद सब कुछ के वह भीतर से बेहद दुखी और अकेली लड़की है...कि उसका बाप जालिम है...कि उसके दोस्त खुदगर्ज़ और मतलबी हैं...कि उसके समाज के लोग छिछले और चालू हैं।...कि उसका बचपन नाना प्रकार की अप्रिय बन्दिशों में बीता है...कि उसके दिल की प्यार की प्यास को आज तक किसी ने नहीं समझा है..कि उससे ज़्यादा बदकिस्मत और मनहूस लड़की दुनिया में शायद ही कोई हो वगैरह।
पन्द्रहवें दिन बड़े रहस्यमयी तरीके से मुझे एक कम्पनी में जूनियर अकाउण्ट्स ऑफिसर का इण्टरव्यू कॉल मिला और बगैर किसी धकमपेल उतने ही रहस्यमयी तरीके से मेरा चयन हो गया और मैं जो रातपाली में प्रेस में काम कर रहा था, दिन में टूयूशनें पढ़ा रहा था, बाक़ी बचे समय में प्रूफ पढ़ रहा था, बाकी बचे समय में खुद भी पढ़ रहा था और बाकी बचे समय में रोमांस कर रहा था और बाकी बचे समय में अपनी आज की ज़िन्दगी को ही जैसे सिनेमा के परदे पर चलता देख रहा था...महीने भर बाद एक दिन अचानक अपहृत करके पास के एक शहर में ले जाया गया और बगैर ज़्यादा ढोल-ढमाके के पति बना दिया गया।
लेकिन यहीं से कहानी का करुण मोड़ आरम्भ हो गया। शादी होते ही स्निग्धा को लग गया कि उसने ग़लत निर्णय ले लिया है। जैसे मुँह से ग़लत बात निकलते ही हमें लग जाता है कि ग़लत बात निकल गयी, लेकिन उसे वापस लेने का कोई उपाय शेष नहीं रहता, फिर तो सिर्फ़ उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार होना होता है, उसे लग गया कि हँसी-हँसी में भयंकर भूल हो गयी है। शादी के दौरान ही उसका मुँह लटक गया, आँखों में चमक की जगह चिन्ता आ बैठी, चेहरे की थिरक और पुलक ग़ायब हो गयी...उसके व्यक्तित्व में जो कुछ भी मोहक और मादक था...देखते ही देखते कपूर की तरह उड़ गया और वहाँ एक निरीह-मजबूर ठगी-घिरी-जीव थी थी....अनजान जगह में जिसकी आख़िरी बस चूक गयी हो...या बीच धार जिसकी नाव में बड़ा सा सुराख हो गया हो या हाथ से चप्पू छूटकर लहरों में बह गया हो....या मेले में जिसकी जेब कट गयी हो...या ऑपरेशन के दौरान जिसकी नाक से ऑक्सीजन की नली निकल गयी हो।
शायद बदला लेने या दुनिया को दिखा देने के रास्ते यहाँ से आगे कहीं नहीं जाते थे। आगे एक नीरस ज़िन्दगी और रुटीन गृहस्थी थी जो सारी निजता और स्वतंत्रता का एक झटके से हरण कर लेती थी और वरण के सारे विकल्पों का एक साथ समापन कर देती थी। अब आगे चुनने को कुछ नहीं था। अब आगे सिर्फ़ एक अस्पष्ट पगडंडी जो अनिश्चय और आशंका की धुंध में डूबी हुई थी....जिस पर चलना पता नहीं कहाँ ले जा सकता था लेकिन जिससे वापसी के सारे पुल वह स्वयं अभी-अभी अपने हाथों जला चुकी थी।
मैं शादी के लिए तैयार हो गया था-यह कहना भी ग़लत ही होगा। हाँ, मेरा मन शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करने का बन रहा था, यह ज़रूर है। क्योंकि मन ही मन मुझे लालच था कि बड़े घर के साथ रिश्ता जुड़ने से मुझे तरह-तरह के लाभ हो सकते हैं-घाटा तो कोई भी नहीं है और दूसरे, वैसे भी मुझसे शादी कौन करता ?
इस तरह बग़ैर पूरी मानसिक तैयारी के हम पति-पत्नी हो गये।
बचपन की स्मृतियाँ बहुत त्रस्त करने वाली हैं। वह तपती रेतपर निरंतर चलती नंगे पैरों की दौड़ जैसा ही है। मेरे पिताजी एक प्रेस में कम्पोज़ीटर थे। गुजारा मुश्किल से ही चलता था। पाँच बहन-भाइयों में मैं सबसे बड़ा था। पिताजी का, लोग कहते थे, किसी दूसरी औरत से सम्बन्ध था। कई रातें उनकी वहीं बीतती थीं। माँ को कोई रहस्यमयी बीमारी थी। पता नहीं पिताजी को भी ठीक से पता था या नहीं कि माँ को क्या बीमारी है। शायद उन्हें पता होगा, पर वह बताते नहीं थे। इतना ज़रूर है कि बीमारी असाध्य होगी और संक्रामक भी। इसीलिए उसका नाम नहीं लिया जाता था। माँ के सारे बदन में हड्डियाँ निकली हुई थीं। कुछ इस तरह कि वह ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकती थीं। सख़्त बिस्तर पर ज़्यादा देर लेटना भी उनके बस का नहीं था। वह दिन रात कराहती रहती थीं। एक नौकरानी आकर उनके कपड़े धो जाती थी, कभी-कभी उन्हें नहला भी जाती थी या उनका बदन गीले तौलिये से पोंछ जाती थी। बाकी घर के कपड़े छोटी बहन धोती थी। सुना यह भी था कि डॉक्टर गिज़ा के लिए कहते हैं, आबोहवा बदलने के लिए कहते हैं
।
दोनों चीज़े हमारे बस में नहीं थीं। एक बार किसी ने कहा कि कबूतर का शोरबा पिलाओ, पर यह भी संभव नहीं था, क्योंकि माँ शाकाहारी थीं। वह दवा भी मुश्किल से ही पीती थीं। उन्होंने अपने तिल-तिल करके मरने को चुपचाप स्वीकार कर लिया था। वह भगवान का नाम भी नहीं लेती थीं। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत भी होती तो हमें नहीं पुकारतीं। पुकारतीं भी तो उनकी कमज़ोर आवाज़ किसी तरह हम तक नहीं पहुँचती। हम ही बीच-बीच में उनके कमरे में जाकर पूछ आते-माँ, कुछ चाहिए ?
माँ को देखकर कभी नहीं लगा कि उनके मन में कोई अतृप्त इच्छा अटकी होगी। उन्हें बस दो ही बातों का अफसोस था। एक-ठाकुरजी सेवा नहीं कर पातीं और दो बच्चों को कुछ बनाकर खिला नहीं पातीं। घर में तो नहीं, पर बाद में अस्पताल में जब हम माँ को देखने या खिचड़ी वगैरह देने जाते-उनकी आँखों में हमें प्यार करने की एक गहरी ललक छटपटाती नज़र आती। हम उसे ठीक से समझ नहीं पाते। माँ तब बहुत दिनों से हमारे दैनिक सुख-दुख से बाहर थीं इसलिए वह हमारे लिए जैसे दूर की कोई रिश्तेदार हो गयी थीं। एक बार उन्होंने अपना हड्डी-हड्डी हाथ मेरे सिर पर फेरकर पूछा-तू कौन सी क्लास में आ गया ? लेकिन जब मैंने बताया तो मानो उन्होंने सुना ही नहीं।
माँ कोई बहुत अच्छी कुक नहीं थीं। बीमारी की वजह से हमें कुछ बनाकर खिलाने का अवसर उन्हें कम ही मिलता था। फिर भी कभी-कभी खासकर, वार-त्यौहार वह अपनी सारी ताकत लगाकर उठतीं और रसोई में आ जातीं। लेकिन रसोई उनकी पसन्द की नहीं होती ! वहाँ कुछ भी अच्छा पकाने के वातावरण का अभाव रहता। या तो मसालदान खाली होता या आटे के पीपे का पेंदा दिखाई दे रहा होता या जूठे बरतन भिनक रहे होते या स्टोव में केरोसीन इतना कम होता कि वह बार-बार भभक या बुझ रहा होता। सफाई तो नहीं ही होती। हम बहन-भाइयों द्वारा की गयी टालमटोल सफ़ाई माँ के लिए गन्दगी लीप देने का ही पर्याय होती। कभी जब सारी चीजें अनुकूल होतीं तो माँ की हँफनी और चक्कर और बाँयठे और अँधेरी उन्हें ज़्यादा देर बैठने नहीं देती। अनुष्ठान की तरह आरम्भ किया पाकप्रयास उन्हें बीच राह बेटी के हवाले कर फिर अपनी खटिया की शरण लेनी पड़ती। फिर भी कभी-कभी वह बड़ी कड़ाही में आटे का घोल उबलवातीं और उसमें ढेर सारा गुड़ का पानी मिलाकर एक तरह की मीठी लेई बनवा देतीं। कहना न होगा कि हम लोग न सिर्फ़ उसे खुश होकर खाते, बल्कि देर तक चाट-चाटकर खाते और उसके लिए लड़ते भी। हम उसे खाना भी चाहते और यह भी नहीं चाहते कि वह खत्म हो जाए। दूसरे दिन भी उसी की बात करते।
घर में मेहमान आये एक अर्सा हुआ था। लेकिन बड़े-बच्चों जैसे मैं और मेरी बहन के मन में मेहमान आने की स्मृति सुरक्षित थी। मेहमानों की स्मृति का सीधा संबंध खाने से था। उन्हें अच्छा खाना खिलाया ही जाता था। वह कुछ-कुछ मात्रा में हमें भी मिल जाता था। कोई-कोई मेहमान अपने साथ किसी एक को घुमाने भी ले जाते थे-लोकल गाइड की बतौर। तब आइसक्रीम, चाट या सोडावाटर का मिलना निश्चित था। घर से निकलने से पहले ही इन क्षणों की प्रतीक्षा शुरू हो जाती थी। जब वे लोग कुछ खाएँगे-पिएँगे और हमें भी मिलेगा। घर लौटकर उत्सुक भाई-बहनों को बताते कि क्या-क्या मिला। कभी-कभी तो हम खुद मेहमानों को बताते चलते कि अमुक दुकान की आइसक्रीम बहुत प्रसिद्ध है और फलाँ ठेलेवाले की चाट बाहर से जो आता है, एक बार ज़रूर खाता है।
इसलिए हमारे दोस्त भी वही थे जो बीच की छुट्टी में हमें अमरूद, ककड़ी, नमकीन वगैरह खिला सकें, या जिनके घर जाओ तो कुछ न कुछ खाने को मिले। बल्कि हम उनके दोस्त क्या, चमचे थे। मैं तो था ही। मैं हर लड़ाई में उनका पक्ष लेता, दौड़-दौड़कर उनका काम करता, उनका होमवर्क कर देता और उनका बैग, उनके जूते तक उठाकर चलता। वे जानते थे। वे करवाते। उन्हें मज़ा आता। मुझे झेंप लगती। फिर भी करता। दोस्तों के घर रोज़-रोज़ खाने पीने में शर्म लगती, क्योंकि जवाब में उन्हें कभी अपने घर बुलाकर कुछ नहीं खिला सकता था-फिर भी रोज़ जाता और जानबूझ कर ऐसे टाईम जब उनका खाने, नाश्ते या दोपहरी का वक़्त हो, एक बार एक दोस्त की मम्मी ने पूछ भी लिया-क्यों रे ? तेरी मइया तुझे कुछ नहीं खिलाती ? भूखा रखती है ? दिनेश के हिस्से का खाने आ जाता है ? सुनकर कान जलने लगे। बाहर आकर अपने ही हाथों से अपने गालों पर दो झापड़ मारे और सारे रास्ते खूब रोया। दूसरे दिन दिनेश ने माफी भी माँगी, पर फिर उसके घर कभी नहीं गया।
सब्ज़ी ख़रीदकर लाने के लिए हम दोनों भाई तैयार रहते थे। सब्ज़ी लाने मण्डी जाना पड़ता था। पैदल। तीन किलोमीटर। लौटते समय दो बड़े और भरे थैले दोनों हाथों में उठाकर लाने पड़ते थे। हाथ दुख जाते थे। सो भी शाम के वक्त। जब मालनें उठनेवाली हों और सारी बची खुची सब्ज़ी सस्ते दाम खाली कर घर जाने के मूड में हों। यानी उस दिन अपने खेल का भी बलिदान। लेकिन सब्ज़ी में से आराम से दस पैसे मारे जा सकते थे। दस पैसे में तीन गोलगप्पे आते थे, या दो नानखटाई या चार लेमनचूस या आठ मीठी गोली या एक चूरन की पुड़िया। गोलगप्पेवाला नखरे लगाता। सारी भीड़ को निबटाकर फिर ध्यान देता। पैसे पहले माँगता। हाथ में लेकर उलट-पटल कर देखता कि खोटा तो नहीं है। फिर गोलगप्पे देता-जिन्हें जल्दी-जल्दी खा लेना पड़ता कि कोई जान पहचानवाला देख न ले-फिर और खाली पानी माँगते, दो बार-वह उसमें भी नखरे लगाता। लेकिन रोज़-रोज़ बेस्वाद फीकी खिचड़ी या सूखी रोटी निगलनेवाली ज़बान को तो इतने से स्वाद से भी मजा आ जाता।
कुछ बड़ा हुआ तो चोरी शुरू कर दी। तरकीब आसान थी। बड़े लड़कों के साथ अँधेरा होने तक फुटबॉल खेलते। खेल ख़त्म हो जाने पर मैदान पर कहीं भी घेरा बनाकर बैठ जाते और गपशप करते। मैदान के साथ-साथ चलती सड़क से बैलगाड़ियाँ गुजरतीं। बड़े लड़के मौक़ा ताड़कर किसी भी बैलगाड़ी के पीछे लग जाते और पीछे से चढ़कर जो जितना हाथ में आये, भर-उठा लाते। कभी गन्ना, कभी फूलगोभी कभी गुड़ की भेली, कभी मूली, कभी मूँगफली। मूँगफली सब बाँटकर खाते। कुछ रोज बाद मुझसे कहा गया। ललकारा गया। मैं गया दबे पाँव। चलती गाड़ी पर चढ़ भी गया, गुड़ था, उठा भी लिया, पर जाने कैसे गाड़ीवाले को पता चल गया। वह चलती गाड़ी से कूद पीछे की तरफ आया। दोस्तों की आवाजें आयीं-साले भाग ! पर मैं कूदने में देर कर गया। गाड़ी चल रही थी। मैं डर गया कि सम्हलकर नहीं कूदा तो गिर जाऊँगा। और सम्हलकर कूदा-कूदा कि गाड़ीवाले ने अपने मजबूत हाथ में मेरी कलाई भींच ली और ज़ोर का झापड़ मारा। मैं बिलबिलाकर रोया, मैंने हाथ की भेली नीचे फेंक दी, मुझे पुलिस में दिये जाने का डर लगा और मेरी निकर में पेशाब निकल आया। मेरी दशा देखकर गाड़ीवाले को हँसी आ गयी और उसने मुझे सिर पर टप्पल मारकर छोड़ दिया। उस दिन सारे दोस्त मुझ पर खूब हँसे। लेकिन धीरे-धीरे एकस्पर्ट हो गया।
मैं भुक्खड़ ! जन्मजात भुक्खड़ ! घर में कोई चीज़ बनवाकर खाता हूँ तो भुक्खड़। कुछ बनाने की फरमाइश करता हूँ तो भुक्खड़। कोई चीज़ अच्छी लगती है और चट कर जाता हूँ तो भुक्खड़ ! बीवी का ख़याल है खा पीकर प्लेट को चाटना या प्लेट को उँगली से पोंछकर उँगली को चाटना भुक्खड़पन होता है। उसका ख़याल है कि प्लेट में जरूर कुछ न कुछ छोड़ना चाहिए। मसलन भजिये बने हों तो चार भजिये खाकर मुझे आप लीजिए, आप लीजिए, करने लगना चाहिए। मुझे मेरे बेटे के आगे एक गन्दी मिसाल की तरह पेश किया जाता है। ‘‘खाओ, ज़रा तमीज़ से अपने पापा की तरह नहीं।’
माँ की बीमारी इस ख़याल से छिपायी जा रही थी कि मोहल्लेवाले या स्कूल के बच्चे हमसे ही छूत न बरतने लगें। लेकिन सारे मोहल्ले को पता था कि माँ मर रही हैं। इसलिए जब वह एक दिन सचमुच मर गयीं तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। धक्का नहीं लगा। खुद हमें भी नहीं। पिताजी ज़रूर रोये। फूट-फूटकर लेकिन उनका रोना देखकर उन पर दया नहीं आ रही थी-गुस्सा आ रहा था। उन्हें एक थप्पड़ रसीद करने की इच्छा हो रही थी।
माँ के मरने के दो महीने बाद एक दिन अचानक पिताजी गायब हो गये। कोई कहता था वह साधु हो गये, कोई कहता था दूसरी औरत के साथ भाग गये। एक पूरे सप्ताह हम पाँचों भाई-बहन उनकी प्रतीक्षा करते रहे और रोते रहे और पड़ोसियों के यहाँ से आयी रोटियाँ खाते रहे और तरह-तरह की योजनाएँ बनाते रहे। मैं भाई-बहनों को समझाता रहा कि हम कोई भी काम कर लेंगे, मेहनत मजदूरी कुछ भी और गुज़ारा चला लेंगे किसी तरह लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगे।
वे अविश्वास से मुझे अपलक देखते और फिर रोने लगते। आठवें रोज़ गाँव से मामाजी आ गये और हम सबको अपने साथ गाँव ले गये। घी दूध का प्रचुरता का लालच देकर। उस साल मुझे दसवीं की परीक्षा देनी थी। गाँव में हम सबके लिए सुबह से रात तक हाड़तोड़ काम था। पढ़ाई का सवाल ही नहीं था। फिर भी छोटे बहन-भाई वहीं रहना चाहते थे। एक दिन मैं वहाँ से भागकर वापस शहर आ गया और उसी प्रेस के आगे जाकर खड़ा हो गया भूखा प्यासा जिसमें पिताजी काम करते थे।
दया करके मुझे रख लिया गया। सुबह-सुबह मैं झाड़ू लगा देता, पानी भर देता, साफ-सफाई कर डालता, चाय-पानी ले आता, चेसिस धो देता, गैली प्रूफ उठा लेता और समय मिलते ही डिस्ट्रीब्यूट करने बैठ जाता। प्रेस के एक पुराने कर्मचारी सीतारामजी टिफिन में मेरे लिए भी दो रोटियाँ डलवाकर घर से ले आते और लंच टाइम में बड़े प्यार से मुझे पकड़ा देते। मैं खा लेता। रात को वहीं जमीन पर चादर बिछाकर सो जाता।
दिमाग तेज़ था। फटाफट काम सीख गया। भाषा अच्छी थी। हिन्दी अंग्रेजी के प्रूफ भी पढ़ देता। एक बार कोई किताब पढ़ लेता तो याद हो जाती। उस साल दसवीं में प्रथम श्रेणी से पास हुआ। प्रेस में ही एक दिन पाटोदिया साहब से मुलाकात हुई। वह चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट थे। कुछ छपाने आये थे। उनके ड्राफ्ट में मैंने एक गलती निकाल दी। हुज्जत करने लगा। डिक्शनरी मँगायी गयी। मैं सही निकला। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा। प्रेममालिक से मेरे बारे में पूछताछ की। चले गये। अगले दिन फिर आये। प्रेसमालिक के पास बैठे। वहाँ मुझे बुलवाया गया। पूछा गया कि क्या मैं पाटोदिया साहब के बच्चों को एक घण्टा पढ़ा दूँगा ?
पाटोदिया साहब का बहुत बड़ा मकान था और बहुत जमी हुई प्रेक्टिस। सम्पन्न व्यक्ति थे। तीन बच्चियाँ थीं। पत्नी शांत हो गयी थीं। माँ घर सम्हालती थीं। वहाँ मुझे अच्छा लगा। बच्चे मुझसे हिल गये। पाटोदिया साहब प्रभावित। प्यार करने की हद तक। मुझे नीचेवाला कमरा दे दिया गया। खाना भी वहीं खाने लगा। कुछ रोज़ बाद दफ्तर के काम में भी उनकी मदद करने लगा। वह कहते थे आदमी मेहनत से जी न चुराये और लगन से काम करे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। हायर सेकंडरी में फर्स्ट डिवीज़न आया। होशियार बच्चे साइंस लेते थे। मैंने कॉमर्स ली। मुझे पाटोदिया साहब जैसा बनना था। लेकिन कमरा बदल लिया। प्रेस की नौकरी छोड़ी नहीं।
बहुत दिन बाद एक दिन अचानक एक दूध की दूकान पर छोटा भाई दिखाई दे गया। आँखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। लिपट गये। वहीं बैठकर बातें करने लगे। भाई ने बताया दो बहनों की शादी हो चुकी है, तीसरी पाँव रपट जाने से कुएँ में गिर गयी और मर गयी। फिर वह मुझसे गाँव चलने की ज़िद करने लगा और मैं उससे अपने घर चलने की। मैं आहत था और उफन रहा था कि मेरी सगी छोटी बहनों के विवाह की मुझे सूचना तक नहीं दी गयी-बगैर यह सोचे कि सूचना कहाँ किस पते पर दी जाती ? भाई घर नहीं आया, मैं गाँव नहीं गया। दोनों पलटकर अपने-अपने रास्ते चले गये।
इसके बाद उसे नहीं देखा।
स्निग्धा ने सोचा था उसकी शादी से शहर भर में हंगामा हो जाएगा। घर में तूफान मच जाएगा और कॉलेज में जिसे पता चलेगा उसका मुँह खुला का खुला रह जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। फिर विश्वास हुआ तो स्निग्धा की बेवकूफी पर तरस आया और लोगों ने उसे मुबारकबाद भी ऐसे दी जैसे सांत्वना दे रहे हों। और तो और किसी ने पार्टी भी नहीं माँगी। इससे वह और दुखी हो गयी और अपने आप पर और ज़्यादा झुँझलाने लगी। इससे उसकी कम हो चुकी सुन्दरता और कम हो गयी। उसने सोचा उसके ग्रुप में न सही उसकी अंतरंग सहेलियों में से तो कोई होगी ही जो उसे इस साहसिक निर्णय की प्रशंसा करेगी, लेकिन यहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगी। अंतरंग सहेलियों की प्रतिक्रिया और ज़्यादा छीलने वाली थी। कम से कम बताना तो था। इतना बड़ा स्टेप ले लिया और एक बार बताया तक नहीं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book