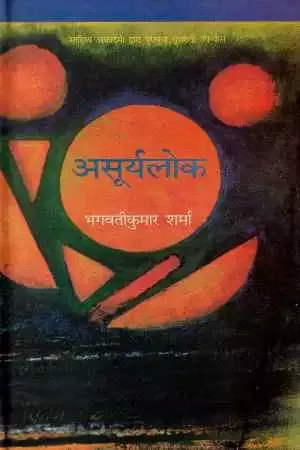|
उपन्यास >> असूर्यलोक असूर्यलोकभगवतीकुमार शर्मा
|
249 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है श्रेष्ठ उपन्यास...
Premchand Ki Atmakatha
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
असूर्यलोक उपन्यास है। ‘पर्जन्य तिलक त्रिवेदी’ या ‘तिलक निगमशंकर त्रिवेदी’या ‘निगमशंकर भद्र त्रिवेदी’-ये नाम किसी नगरपालिका या शाला के दफ्तर में दर्ज नहीं हुए होंगे। अगरचे सत्य कभी कथालोक से अधिक चौंका दें,इस तरह यथार्थ से स्पर्धा करता है। (वैसे यह हुआ भी हो तो भी वह पर्जन्य तिलक या निगमशंकर भिन्न ही होंगे) फिर भी,जब इस उपन्यास को अंत तक पढ़ लेते हैं, तो वासनामय जीवन के कीट के रूप में अंतिम साँस ले रहे भद्रशंकर,ज्ञान में और भागीरथी की आँखों के दीये निहार रहे निगमशंकर, जिन्दगी भर कहीं आँखों में कुएँ तो नहीं बने रहेंगे-इस भय के साथ जी रहा तिलक,एक क्षण में विवाह की पूर्व-रात्रि में अपना सर्वस्य तिलक के चरणों में समर्पित करनेवाली और धरती तथा देव के प्रसाद के रूप में संसार को निभा रही सत्या,ईक्षा गोरधन सेठ और सजल,सत्या के नगर में आगमन के साथ ही सजल का प्राण त्यागना-ये सारी घटनाएँ और सजल के प्राणत्याग के बावजूद उसके कार्य को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प कर रहा कृतार्थ और तिलक के कार्य-क्षेत्र के मधुबन में सत्या ने सामने चलकर माँगे हुए तथा अपने भीतर रोपे हुए और अपने रेगिस्तान में जतन से बड़े किये हुए पारिजात-जैसा पर्जन्य तिलक के मधुबन में महक फैलाना चाहें, तब सत्या के अल्पाधिक सौभाग्य पर सामाजिक सम्मति की मुहर लगा रहे गोरधन सेठ और उपन्यास के कुछ विकट क्षणों में भी उपस्थित रहनेवाले कृष्णजी...आदि पात्र मानो चिरकाल से पहचाने हुए हों,वैसे मन में बस जाते हैं।
भगवती भाई ने सृजनपथ पर की अपनी यात्रा आँखे खुली रखकर की है। उस यात्रा में उन्हें जो पात्र मिल गये,वे इन पृष्ठों का नेत्र प्रवास पूरा होने तक केवल पात्र नहीं रहते हैं।....हाँ,इन सभी पात्रों को मै पहचानता हूँ। आपकी मैं उनसे पहचान कराता हूँ..बहुत कुछ कह सकता हूँ। पर अच्छे लोगों से परिचय करानेवाले बहुत देर रूकते नहीं है। आप उनसे मिल लें। इसके बाद आपका अगर मुझसे मिलना होगा तो आप कहेंगे, ये पात्र तो जैसा आपने कहा था,हमसे भी अधिक जीवंत निकले।
भगवती भाई ने सृजनपथ पर की अपनी यात्रा आँखे खुली रखकर की है। उस यात्रा में उन्हें जो पात्र मिल गये,वे इन पृष्ठों का नेत्र प्रवास पूरा होने तक केवल पात्र नहीं रहते हैं।....हाँ,इन सभी पात्रों को मै पहचानता हूँ। आपकी मैं उनसे पहचान कराता हूँ..बहुत कुछ कह सकता हूँ। पर अच्छे लोगों से परिचय करानेवाले बहुत देर रूकते नहीं है। आप उनसे मिल लें। इसके बाद आपका अगर मुझसे मिलना होगा तो आप कहेंगे, ये पात्र तो जैसा आपने कहा था,हमसे भी अधिक जीवंत निकले।
कृतज्ञता का सूर्य
हेनरी मिलर ने एक पत्र में लिखा था, मैं रोज़ तीन काल में जी रहा हूँ; विगत में, वर्तमान में तथा अनागत में। विगत मेरे लिए गोता-तख़्ता है, वर्तमान पिघलता जाता है और अनागत निरा आनन्द है मैं इन तीनों में एक साथ जी रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ ज्यादा अच्छा लिखूँ तो होंठों से पुचकारते हुए मैं अपने कंधों के पीछे देख लेता हूँ। ईसा के बाद के 2500वें 5000वें वर्ष में जीनेवाले और बीसवीं शताब्दी के महान लेखक हेनरी मिलर को बड़ी रुचि के साथ पढ़ने वाले पाठक के साथ मैं मिल जाता हूँ।
भगवती कुमार शर्मा विनम्र हैं, वे ऐसे शब्द कभी नहीं कहेंगे, किन्तु प्रत्येक सर्जक का अपनी प्रतिभा के साथ एक आंतरिक नाता होता है, वह कुछ कमजोर लेखन कर दे, तब भी उसके भीतर स्पन्दन होता ही है, जैसे सबल सृजन करते समय होता है, असूर्यलोक लिखते समय भगवती भाई के मन में हेनरी मिलर-जैसा ही भाव आया होगा। जो कथाएँ आनेवाले समय तक जीवित रहेंगी, ऐसी ही कुछ समृद्ध रचनाओं में असूर्यलोक को मैं स्थान देता हूँ। मैं यह कहता हूँ कि तब मेरे शब्द मित्र-प्रेम से नहीं, अपितु मेरी यत्किंचित् आलोचनात्मक दृष्टि के प्रभाव से प्रकट होते हैं।
तीन-चार साल पहले रघुवीर चौधरी ने बात-बात में कहा था : 1987 सरस्वतीचंद्र के प्रकाशन का शताब्दी वर्ष है। उसी वर्ष में (कन्हैयालाल) मुंशी की जन्म शताब्दी भी आती है। उस वर्ष में किसी उत्तम कृति का सृजन होना चाहिए। तब से यह प्रतीक्षा थी कि गुजरात के किसी सर्जक की लेखनी से कोई समर्थ कृति मिल जाये। यह साल पूरा होने में अभी ठाई महीने बाक़ी हैं। कोई अन्य कृति मिल जायेगी, ऐसा विश्वास है, परंतु भगवती भाई ने पिछले साल के मध्य में असूर्यलोक के कुछ प्रकरण मेरे हाथ में रख दिये, तभी से मुझे ऐसा लग रहा था कि रघुवीर चौधरी का संकल्प फलीभूत हो रहा है। फिर तो वह कृति जन्मभूमि में प्रवासी धारावाहिक रूप में प्रकाशित होने लगी। पाठकों की प्रतिक्रिया मैं रुचिपूर्वक देखता रहा। भगवती भाई ने शैली के विषय में कहीं भी समझौता नहीं किया है। अपने गद्य की संरचना के और अपने पसन्द किये हुए कथा के माहौल के लिये अनिवार्य जटिल शब्दों का प्रयोग उन्होंने टाला नहीं है। दैनिक पत्र के पाठकों के लिए यह कृति कहीं कठिन तो नहीं बन जायेगी—मुझे यह डर था। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मेरा डर बेबुनियाद निकला। जब नितान्त सुन्दर सर्जक पाठक भी समझ पायें तो इसका आनन्द अनोखा होता है।
छपे हुए 602 पृष्ठ काफ़ी समय से मेरे पास पड़े हुए हैं। दो बार मैं इस कृति के करीब गया हूँ, फिर भी मैं निस्संकोच कह सकता हूँ कि यह ऐसी कृति नहीं है, जिसे कोई एक बार ही पढ़ ले। कई बार ऐसा हुआ है कि कथारस आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। और कथागुम्फन बार-बार पीछे मुड़कर देखने को मजबूर करता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो भावनाओं को आघात देने लगें और समझ में न आए तो उन शब्दों से संबंधित घटना विस्तार से कहाँ घटी थी, यह देखने के लिए पहले के कुछ पन्ने पलटने को मन करेगा ही।
राइट मोरिस ने उपन्यास-लेखन की सृजनात्मक परिभाषा की है : ‘‘कोय रेशम बनाते हैं, ठीक उसी तरह हम कहानियाँ लिखते हैं।’’ आगे वे कहते हैं: ‘‘कहानीकार बनना पादरी बनने की अभिलाषा रखने—जैसा है। पादरी बनने के लिए असंख्य विद्यार्थियों को भर्ती किया जाता है, मगर उनमें से बहुत कम को पसन्द किया जाता है।’’ कथा लेखन में सर्जनात्मकता की जयमाला लेखक की सभी रचनाओं को शाश्वत सुरभि के साथ प्राप्त नहीं होती है। असूर्यलोक में कथागुम्फन लेखक बना रहे कोये-जैसा है। ‘‘तब वह नगर सन्ध्या बेला में डूब रहे सूरज के समान लग रहा था।’’—इस वाक्य से आरम्भ होकर भद्रशंकर, निगमशंकर, तिलक और पर्जन्य तक पहुँचकर चार पीढ़ियों के साठ से अधिक वर्षों की समयावधि में व्यस्त होकर ‘‘जगन्नाथ के रथ के पहियों से किचुड़-किचुड़ आवाज़ निकली। रथ आगे बढ़ा बढ़ता ही रहा’’ जैसे वाक्य के साथ पराकाष्ठा के बिन्दु तक पहुँच रही इस कृति को पूरा पढ़ लेने के बाद यह प्रस्तावना लिखने वाले को विश्वास हो गया कि जिन लोगों का आह्वान किया है और इने-गिने व्यक्तियों को चुना गया है उनमें भगवती कुमार शर्मा अवश्य हैं।
भगवती कुमार शर्मा की सृजनयात्रा का आरम्भ कवि रूप में हुआ, साथ ही वे कहानी, उपन्यास और निबन्ध की विधाओं में भी आगे बढ़ते रहे हैं। एक पत्रकार के रूप में घटना को बाहर से देखना और कवि के रूप में उसे भीतर से अनुभव करना—यह वरदान के साथ ही अभिशाप भी है। इस दृष्टि से भगवतीभाई झवेरचंद मेघाणी या चुनीलाल माड़िया की परम्परा निभा रहे हैं। फिर भी उनकी निजी मुद्रा उभरती है।
असूर्यलोक में भगवतीकुमार अपने अनेक बार दुहराये गये विषय को फिर से ले आते हैं। अनाधिकार—जैसी कहानियों में, समयद्वीप—जैसे उपन्यासों में दिखाये गये संघर्षों की कुछ लकीरें यहाँ भी पायी जाती हैं : विषय का पुनरावर्तन है, लेकिन यहाँ संघर्ष बिलकुल ही भिन्न प्रकार का है। लेकिन जैसे फ्रांसीसी लेखक सेलान ने कहा है :’’
We shall never beat peace, until everything has been said, once for all times.’’
भगवतीकुमार जो कहना चाहते हैं, उसके लिए कहानी या लघु उपन्यास का ढाँचा छोटा पड़ रहा था। सशक्त संरचनावली कृति में कभी-न-कभी इसे प्रकट होना ही था। उत्तम कलाकृति के प्रथम प्रयोग के पहले ग्रांड रिहर्सल में इसे विविध अंशों में उभारना संभव हुआ था। पहले की कृतियों में समय और स्थल के परिणाम भिन्न थे। असूर्यलोक में समय और स्थल के परिणाम सूक्ष्म रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। मध्यकालीन युग के पहले से यूरोप के साहित्य में ‘सागा’’’ (अनेक पीढ़ियों तक फैलती इतिहासगाथा) लिखने की प्रणाली थी। हमारे यहाँ रघुवंशम् भी एक ‘‘सागा’’ ही है। गाल्सवर्दी ने अपनी कृति फोरसाइट सागा द्वारा इस कथारूप को सामाजिक सन्दर्भ दिया है। जैसा कि पश्चिम के एक समीक्षक ने कहा है, क्या कब घटा है, इसकी बात कहना आरम्भ करें, तब वह इतिहास होता है। क्यों और कैसे वह घटा, यह कहने लगे, तब उपन्यास बन जाता है। भगवतीकुमार ने सागा की इतिहास शैली अपनाकर उसे कथा के रूप में कालस्वरूप दे दिया है।
शीर्षक से ही कृति का रस घुटने लगता है। पहले ही प्रकरण में ईशावास्य के ‘असूर्या नाम ते लोका’ के साथ उलझता नहीं है। उस श्लोक में ‘असूर्य’ और ‘लोक’ दोनों शब्द हैं लेकिन यह असूर्य लोक वह नहीं है, जो भगवती कुमार को अभिप्रेत है। असूर्यलोक की पहचान तो आरम्भ के पृष्ठों में नगर के वर्णन में ही मिल जाती है। ‘‘धुएँ की उन छोटी, नीची दीवारों को फांदकर डगमग गुज़र रही सँकरी सड़कें, ऊबड़-खाबड़ लेकिन ख़ामोश सड़कें...सर्दियों की शाम जैसी या लालटेन के धब्बेदार गोले, जैसी धुँधली धब्ब आँखें, धुँधले अक्षरों में लिखा गया डॉ. श्रीधर तांजोरकर (के नाम) का बोर्ड नगर की कुहासे भरी छवि में पूर्णतया एकरूप हो गया था, उन क्षणों पर वर्षों के उपले-कंडों की राख जम गयी थी, जगमगाते हुए क्षणों में काले भालू के लहू के मोटे लट्ठ रेले की तरह अचानक ही अँधेरा छा गया, भरी दुपहर में भी दिशाएँ मैली धुँधली। अम्बा माँ ने पोस्टकार्ड बढ़ाया। निगमशंकर ने टटोलकर उसे हाथ में लिया, आँखों के सामने रखा, लेकिन अक्षर सारे अंतर्धान !’’ ‘‘तुम अपनी पढ़ाई भूल गए या फिर तुम्हारी आँखों में कुँए खोद दिये गये हैं ?’’ ‘‘टटोलना, यही क्या जीवन का पर्याय बना रहेगा ?’’ ‘‘सूबह की धूप फैलते-फैलते ही सिमट गयी।’’ यहाँ तक अन्धकार आवृत होने के कारण अंध असुरों के लोक का सन्दर्भ रहता है, परंतु सोलह साल की उम्र में जिसने अचानक ही आँखें खोल दी थीं, उस निगमशंकर से पण्डित विनोदानन्द झा पूछते हैं, ‘‘बन्धु, तुम पढ़ने के लिए काशी चलोगे ?’’ भगवती कुमार आगे लिखते हैं : ‘‘काशी ? निगमशंकर रोम-रोम से आन्दोलित हो उठे। उन्हें ऐसा लगा कि उनका अनधत्व दूर हो गया था और किसी मन्दिर के गुम्बद के स्वर्णकलश जैसा प्रकाश चारों ओर फैल गया था। मानो वे पंडित विनोदानन्द झा का चेहरा देख सकते थे और पोथियों में सामवेद के मंत्रों के अक्षर और स्वर भी दिखायी देने लगे थे। कुछ समय से माँ का जो मुख देख नहीं पा रहे थे, वह भी (आँखों के सामने) झिलमिला उठा और अम्बा माँ ने भरी दोपहरी में पढ़कर सुनाने को जो पत्र दिया था, वह भी पुनः साकार हो उठा और अब तो उस पत्र का हर अक्षर....’’ यहीं इस अंतिम वाक्य में आगे के छह सौ पृष्ठों में भगवतीभाई जिसकी बात करने जा रहे हैं उस ‘असूर्यलोक’ का प्रथम दर्शन होता है।
उपर्युक्त उद्धरणों में सहज रूप से ही लेखक की शैली के कुछ उदाहरण मिल गये हैं। भगवतीभाई की इसके पहले की कृतियों की भाषा के साथ इनकी तुलना करनी चाहिए। डब्ल्यू.बी. यीट्स अपने एक नाटक की प्रस्तावन में कहते हैं : ‘‘जैसे मैंने अपने वाक्य-विन्यास, कारक प्रक्रिया को बदला, वैसे ही अपनी प्रज्ञा को भी नया रूप दिया। (As I altered my syntax, I altered my Intellect) भगवतीकुमार अपनी कारक प्रक्रिया को बदलते हैं और प्रथम प्रकरण से ही इनकी प्रतीति हो जाती है। जब लेखक एक ही ढंग से लिखता रहता है, एक ही ढंग से पात्रों को ढालता है, तब उसमें वैविध्य होने पर भी गति नहीं होती है। यहाँ हम प्रज्ञा को, सर्जकता को नया रूप देने वाली कारक प्रक्रिया के साक्षी बनते हैं।
भगवती कुमार यहाँ अपनी वैविध्यपूर्ण विरासत को निरूपित करते हैं। जन्म से और कर्म से ब्राह्मण होने के कारण वे वैयक्तिक ढंग से बड़े हुए। एकओर आसपास के वातावरण आदि से आनेवाली विरासत है, तो दूसरी ओर वह विरासत है जो भारतीय संस्कृति के मूल्यों को लेकर टिकी हुई है। यो दोनों विरासतें उनकी सर्जकता के बिन्दु में एक रूप हो जाती हैं। उनके पास वे सत्य हैं जो अभिव्यक्त होने के लिये व्याकुल हैं। पहले भी अपूर्ण रूप से वे सत्य अभिव्यक्त होते रहे हैं। अब वे सभी सत्य उनके द्वारा समग्र रूप से प्रकट होने के लिये अधीर हो रहे हैं। यहाँ यथार्थ का निरूपण नहीं है, अपितु अनुभव लोक की प्रतिष्ठा है। यह अनुभव लोक यथार्थ पर आधारित है। कथासाहित्य में निहित सत्य जीवन के सत्य की अपेक्षा अधिक यथार्थपूर्ण होता है। फिर एक बार उपन्यास के स्वरुप के विषय में गंभीर रूप से चिंतन करने वाले राइट मोरिस का स्मरण हो आता है। वे कहते हैं : ‘‘हम यथार्थ के आधार पर जीने की कोशिश करते हैं, परन्तु जीने का उद्यम तो कथा साहित्य में ही करते हैं। केवल कथालोक ही जीवन के यथार्थ को पूर्णरूप से अपने में समा लेता है।’’
असूर्यलोक उपन्यास है। ‘पर्जन्य तिलक त्रिवेदी’ या ‘तिलक निगमशंकर त्रिवेदी’ या ‘निगमशंकर भद्रशंकर त्रिवेदी’—ये नाम किसी नगरपालिका या शाला के दफ़्तर में दर्ज नहीं हुए होंगे। अगरचे सत्य कभी कथालोक से अधिक चौंका दे, इस तरह यथार्थ से स्पर्धा करता है। (वैसे यह हुआ भी हो, तो भी वह पर्जन्य, तिलक या निगमशंकर भिन्न ही होंगे।) फिर भी जब इस उपन्यास को अंत तक पढ़ लेते हैं, तो वासनामय जीवन के कीट के रूप में अंतिम साँस ले रहे भद्रशंकर, ज्ञान में और भागीरथी की आँखों के दीये निहार रहे निगमशंकर, ज़िन्दगीभर कहीं आँखों में कुएँ तो नहीं बने रहेंगे—इस भय के साथ जी रहा तिलक, एक क्षण में विवाह की पूर्व-रात्रि में अपना सर्वस्व तिलक के चरणों में समर्पित करनेवाली धरती तथा देव के प्रसाद के रूप में संसार को निभा रही सत्या, ईक्षा, गोरधन सेठ और सजल, सत्या के साथ पुनर्मिलन के समय ही तिलक की आँखों की दृष्टि का विलीन हो जाना और सत्या के नगर में आगमन के साथ ही सजल का प्राण त्यागना—ये घटनाएँ और सजल के प्राणत्याग के बावजूद उसके कार्य को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प कर रहा कृतार्थ और तिलक के कार्य-क्षेत्र के मधुवन में सत्या के सामने चलकर माँगे हुए तथा अपने भीतर रोपे हुए और अपने रेगिस्तान में जतन से बड़े किये हुए परिजात-जैसा पर्जन्य तिलक के मधुवन में महक फैलाना चाहें, तब सत्या के अल्पाधिक सौभाग्य पर सामाजिक सम्मति की मुहर लगा रहे गोरधन सेठ और उपन्यास के कुछ विकट क्षणों में ही उपस्थित रहनेवाले कृष्णजी...(महाभारत में कृष्ण द्वैपायन कर्ता भी हैं और कथा के पात्र भी, किंतु यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि कहीं-कहीं सर्जक स्वयं कर्ता और पात्र के रूप में तो नहीं आ गये हैं ?) आदि पात्र मानो चिरकाल से पहचाने हुए हों, वैसे मन में बस जाते हैं।
अन्य पात्रों के बारे में भी कहा जा सकता है। पर इतने पात्रों की भी पूरी पहचान कहाँ दे पाया हूँ ?
भगवती कुमार ने इन पात्रों को जीवन का परिमाण दिया है। कहते हैं कि सर्जक कोई समस्या पैदा कर दे और उसका हल भी ला दे, इसके साथ ही वह इस धरती पर के जीवनसत्य का दर्शन कराता है। भगवतीकुमार ने असूर्यलोक के तेजोमय रूप को प्रकट करने वाले कुछ जगमगाते पात्रों का सृजन किया है। उन्हें केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी आकार दिया है। जेम्स जॉयस ने कहा है;
‘‘Any man of real individuality tries to know and to understand what is happening, even in himself, as he goes along.’’
भगवतीभाई ने सृजन पथ पर अपनी यात्रा आँखें खुली रखकर की है। उस यात्रा में उन्हें जो पात्र मिल गये, वे इन छह सौ पृष्ठों का नेत्र प्रवास पूरा होने तक केवल पात्र नहीं रहते हैं। मैं आपको अचूक पहचान दे सकता हूं। यह तिलक, इससे आप मिले नहीं हैं क्या ? स्थूल महत्त्वाकांक्षा को त्यागकर केवल ग्रंथालय में प्रज्ञा के बीच ही रहना जिसे पसन्द था, वह अनूठा युवक—और यह सत्या, चंचल और अनर्गल प्रेम करने वाली, दुनिया के प्रति बेपरवाह, फिर भी परिस्थितियों की परिसीमा को अखण्डित रखकर जीनेवाली आसाधारण नारी...हाँ, इन सभी पात्रों को मैं पहचानता हूँ। आपकी मैं उनसे पहचान कराता हूँ; बहुत कुछ कह सकता हूँ। पर अच्छे लोगों से परिचय कराने के बाद से परिचय करानेवाले बहुत देर तक रुकते नहीं हैं। आप उनसे मिल लें इसके बाद आपका अगर मुझसे मिलना होगा तो आप कहेंगे; ‘‘ये पात्र तो जैसा आपने कहा था, हमसे भी अधिक जीवंत निकले !’’ केवड़े की सुगंध की भाँति प्रवेश कर रही निगमशंकर की नयी माँ से लेकर उपन्यास पराकाष्ठा के बिन्दु तक पहुँचता है, तब तक आनेवाले सभी पात्रों के बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं चाहे कितना भी कहूँ, इन पात्रों से मिलने के बाद आप मुझसे कहेंगे : ‘‘अरे, इन सबके बारे में आपने कुछ कहा ही कहाँ है ?’’
भगवती भाई,
आपसे दो बातें कहनी हैं। मुझे विश्वास है कि उपन्यास पढ़ लेने के बाद अनेक पाठक इसके नीचे अपने हस्ताक्षर करने को प्रेरित होंगे। चित्त को प्रसन्न कर दे, ऐसी सशक्त रचना देने के लिए अपने शब्दों द्वारा मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उत्तम सृजन करने वाले सर्जक के प्रति कृतज्ञता का सूर्य हृदय में जगमगाता ही रहता है।
इस कृति ने मेरा भी निर्माण किया है
हालाँकि इस उपन्यास का धुँधला-सा विचार तंतु 1984 के दिसम्बर या 1985 के जनवरी में पहली बार मेरे मन में प्रकट हुआ था, किंतु वास्तव में असूर्यलोक का बीज लेकर ही मैं पैदा हुआ था। कोई दस साल की उम्र में आँखों पर पहली बार चश्मा लगा, तब से अन्तर्मन में जो बीज बोया गया होगा, उसे करीब साढ़े चार दशकों के बाद इस उपन्यास में वृक्ष का रूप में प्राप्त हुआ है। 1985 में कई महीने में असूर्यलोक का लेखन आरम्भ करके कोई दो महीने में उसे पूरा कर दिया, तब मैं आनन्दविभोर हो गया। जब उसका पुनर्लेखन करना शुरू किया तो हर शब्द मुझे चुनौती देने लगा। फिर भी दो-तिहाई कार्य तो पूरा कर ही दिया। फिर गंभीर बीमारी के कारण तीन महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ा। निष्क्रियता के उस कालखण्ड में उपन्यास और कथालेखन का भीतरी लय टूट गई। पात्र, घटनाएँ, निरूपण—इनके बारे में मन में अनेक प्रश्न उठे। अनेक नये बिन्दु भी सूझ गये। स्वास्थ्य ठीक होने पर पांडुलिपि को फिर से हाथ में ले लिया। लेकिन मन दृढ़तापूर्वक इंकार करने लगा—यह नहीं चल सकता।’’ ‘और पुनश्च हरिओम’ करके असूर्यलोक तीसरी बार आरम्भ किया जो 1986 के नवम्बर तक पूरा किया। केवल यह हुआ कि पहले और तीसरी बार के लेखन के बीच उपन्यास का हृदय तो टिका रहा, परंतु इसे छोड़कर पूरा ढाँचा ही बदल गया। इस उपन्यास की रचना—प्रक्रिया में मेरी धृति की बड़ी भारी कसौटी हो गई। साथ ही इस उपन्यास ने मेरे हृदय की श्रद्धा का भी पुनर्निर्माण किया। इसे लिखने के पहले मैं जो था, वह काफी हद तक इसे लिख लेने के बाद नहीं रह गया होऊँगा।
आसूर्यलोक को बम्बई के प्रसिद्ध साप्ताहिक जन्म-भूमि में धारावाहिक रूप में प्रकट होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। इसका सारा यश उस पत्र के सम्पादक और विख्यात कवि और साहित्यकार श्री हरीन्द्र दवे को है। उन्होंने तथा उनके सहकारी श्री हिम्मत भाई मेहता, श्रीत्र्यंबक महेता, प्रताप के संपादक श्री जगदीश शाह, तरु बहन कजीरिया, भाई विनीत शुक्ल और अन्य व्यक्तियों ने इस कृति के प्रति सद्भाव व्यक्त किया। उन सबका मैं ऋणी हूँ। हरीन्द्र भाई ने जन्मभूमि-प्रवासी में असूर्यलोक के समापन के समय अत्यंत उत्साह भरे शब्द लिखे और बाद में इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखने का मेरा अनुरोध भी माना। उनका यह बन्धुकृत्य मेरे जीवन की एक मधुरतम स्मृति बनकर रहेगा। उनके ऋण-स्वीकार के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं।
असूर्यलोक के धारावाहिक प्रकाशन को पाठकों का जो अपार प्रेम प्राप्त हुआ है, यह भी मुझे धन्य करने वाला अनुभव था। आदरणीय श्री उमाशंकर जोशी, श्रीमती कुन्दनिका कापडीआ, श्री शिवकुमार जोशी, श्री दिलीप राणपुरा, श्री जयंतीलाल महेता, श्री प्रकाश न. शाह आदि सारस्वतों ने इस कृति में रुचि लेकर मुझे स्नेहसिक्त किया, इसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ।
लंदन के वयोवृद्ध समीक्षक लेखक माननीय श्री भानुशंकर ओ. व्यास ने तो असूर्यलोक को अपनी ही कृति मानकर लंदन से उस पर वात्सल्य की वर्षा की। इस पुस्तक के सन्दर्भ में उनके लिखे हुए पत्रों की एक स्वतंत्र पुस्तक बनाई जा सकती है। इन पत्रों का एकाध अंश इस पुस्तक में शामिल कर दिया है। मेरे लिए भानुभाई का सौजन्य अविस्मरणीय है। दुर्भाग्य से वे इस पुस्तक को देख पायें, इसके पहले उनका दु:खद निधन हो गया।
मुझे बार-बार ऐसा लगता है कि किसी अगम्य तत्व ने मुझे इस उपन्यास को लिखने के लिए प्रेरित किया है। अनेक व्यवधानों के होते हुए भी यह उपन्यास परिपूर्ण हो सका, इसके लिए मुझे परम तत्व के संचरण का विनीत भाव से आभारी होना चाहिए विख्यात अध्यात्मचिंतक डॉ. कांतिलाल कालाणी के आशीर्वाद इस कृति के सृजन के दरम्यान मुझे प्राप्त होते ही रहे हैं। ‘‘आप जब उपन्यास लिख रहे थे, तब मैं आपके साथ ही था।’ उनके ये शब्द मेरे जीवन की अनमोल संपत्ति हैं। अपने संतोष, प्रेरणा और अवतरणों के विषय में मैंने डॉ. कलाड़ी का तथा कवि श्री मकरन्द दवे के ग्रन्थ विष्णु सहस्रनाम : आंतरप्रवेश का आधार लिया है। इन दोनों महानुभवों के आगे मैं प्रमाणित करता हूँ ।
इसके अतिरिक्त असूर्यलोक के नामकरण में सहायरूप बननेवाले भाई कपिल देव शुक्ल, इस उपन्यास में आने वाली नेत्ररोग से सम्बन्धित चर्चा में अधिकृत जानकारी देनेवाले सूरत के मशहूर नेत्रचिकित्सक डा. के.के. देसाई, ज्यां पाल सार्त्र के अवतरणों के लिए उनकी साक्षात्कार की पुस्तिका के अनुवादक आदरणीय श्रीगुलाबदास ब्रोकर, मुझे यह उपन्यास लिखने की सुविधा प्रदान करने वाले मेरे मित्र श्रीनानूभाई नायक, जनक नायक और सौभाग्यवती जयश्री नायक, इस कृति की प्रतियोंके जतन में सहायक होनेवाले प्रो. मुकेश कॉन्ट्रेक्टर, श्री दिनेश अनाजवाला, असूर्यलोक के लेखन में आदि से अंत तक मेरे साथ रहने वाली मेरी पुत्री चि. रीना, मेरे सभी स्वजन सौ. ज्योति, चि.मेहूला, सौ. झरना, चि. रुचिरा, श्री चंद्रकांत भाई पांड्या, मेरे मिक्त्र मनहर भाई चौक्सी, नयन देसाई रवीन्द्र पारेख, बकुलेस देशाई, और प्रसिद्ध समीक्षक श्री कृष्णवीर दीक्षित—इन सबके प्रति मैं हृदयपूर्वक आभार प्रकट करता हूँ। असूर्यलोक में निगमशंकर को जो अंधत्व आता है, उस घटना का प्रज्ञाचक्षु पंडित सुखलाल जी के जीवन की एक ऐसी घटना के आधार पर निरूपण किया है। निगमशंकर के ग्रंथ भंडार का बाढ़ में नष्ट हो जाना—इससे मिलती-जुलती घटना बरसों पहले श्री कांति भडिया के एक सुंदर नाटक में देखी थी, ऐसा कुछ स्मरण है।
ऊर्ध्वमूल के लेखन-प्रकाशन के बहुत ही लम्बे समय के बाद असूर्यलोक उपन्यास आया है। ऊर्ध्वमूल को पाठकों-समीक्षकों का विपुल प्रेम प्राप्त हुआ था। असूर्यलोक के सम्बन्ध में इसका पुनरावर्तन होगा तो मेरा सृजनश्रम सार्थक हो जायेगा। सरस्वतीचंद्र जैसे हमारे ग्रंथ मणि के प्रकाशन की और कन्हैयालाल मुंशी जैसे हमारे समर्थ उपन्यासकार की जन्म शताब्दी के वर्ष में असूर्यलोक का प्रकाशन हो रहा है, उस सुखद संयोग से धन्यता का अनुभव करता हूँ। मुझे यह निखालिस भाव से कहना चाहिए कि असूर्यलोक मैंने लिखा है, इससे अधिक तो इस कृति ने साथ-ही-साथ मेरे भीतर लक्ष-लक्ष में अक्षर अंकित किये हैं। सर्जक कृति का निर्माण करता है, कृति भी सर्जक का आंतरिक निर्माण कर सकती है, इस रचना की सृजन-यात्रा से मुझे यह अनुभव हुआ है, इस लीला के नियंता ऐसे परम तत्व के चरणों में सिर झुका कर यह कृति आप सबको सादर समर्पित करता हूँ।
भगवती कुमार शर्मा विनम्र हैं, वे ऐसे शब्द कभी नहीं कहेंगे, किन्तु प्रत्येक सर्जक का अपनी प्रतिभा के साथ एक आंतरिक नाता होता है, वह कुछ कमजोर लेखन कर दे, तब भी उसके भीतर स्पन्दन होता ही है, जैसे सबल सृजन करते समय होता है, असूर्यलोक लिखते समय भगवती भाई के मन में हेनरी मिलर-जैसा ही भाव आया होगा। जो कथाएँ आनेवाले समय तक जीवित रहेंगी, ऐसी ही कुछ समृद्ध रचनाओं में असूर्यलोक को मैं स्थान देता हूँ। मैं यह कहता हूँ कि तब मेरे शब्द मित्र-प्रेम से नहीं, अपितु मेरी यत्किंचित् आलोचनात्मक दृष्टि के प्रभाव से प्रकट होते हैं।
तीन-चार साल पहले रघुवीर चौधरी ने बात-बात में कहा था : 1987 सरस्वतीचंद्र के प्रकाशन का शताब्दी वर्ष है। उसी वर्ष में (कन्हैयालाल) मुंशी की जन्म शताब्दी भी आती है। उस वर्ष में किसी उत्तम कृति का सृजन होना चाहिए। तब से यह प्रतीक्षा थी कि गुजरात के किसी सर्जक की लेखनी से कोई समर्थ कृति मिल जाये। यह साल पूरा होने में अभी ठाई महीने बाक़ी हैं। कोई अन्य कृति मिल जायेगी, ऐसा विश्वास है, परंतु भगवती भाई ने पिछले साल के मध्य में असूर्यलोक के कुछ प्रकरण मेरे हाथ में रख दिये, तभी से मुझे ऐसा लग रहा था कि रघुवीर चौधरी का संकल्प फलीभूत हो रहा है। फिर तो वह कृति जन्मभूमि में प्रवासी धारावाहिक रूप में प्रकाशित होने लगी। पाठकों की प्रतिक्रिया मैं रुचिपूर्वक देखता रहा। भगवती भाई ने शैली के विषय में कहीं भी समझौता नहीं किया है। अपने गद्य की संरचना के और अपने पसन्द किये हुए कथा के माहौल के लिये अनिवार्य जटिल शब्दों का प्रयोग उन्होंने टाला नहीं है। दैनिक पत्र के पाठकों के लिए यह कृति कहीं कठिन तो नहीं बन जायेगी—मुझे यह डर था। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मेरा डर बेबुनियाद निकला। जब नितान्त सुन्दर सर्जक पाठक भी समझ पायें तो इसका आनन्द अनोखा होता है।
छपे हुए 602 पृष्ठ काफ़ी समय से मेरे पास पड़े हुए हैं। दो बार मैं इस कृति के करीब गया हूँ, फिर भी मैं निस्संकोच कह सकता हूँ कि यह ऐसी कृति नहीं है, जिसे कोई एक बार ही पढ़ ले। कई बार ऐसा हुआ है कि कथारस आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। और कथागुम्फन बार-बार पीछे मुड़कर देखने को मजबूर करता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो भावनाओं को आघात देने लगें और समझ में न आए तो उन शब्दों से संबंधित घटना विस्तार से कहाँ घटी थी, यह देखने के लिए पहले के कुछ पन्ने पलटने को मन करेगा ही।
राइट मोरिस ने उपन्यास-लेखन की सृजनात्मक परिभाषा की है : ‘‘कोय रेशम बनाते हैं, ठीक उसी तरह हम कहानियाँ लिखते हैं।’’ आगे वे कहते हैं: ‘‘कहानीकार बनना पादरी बनने की अभिलाषा रखने—जैसा है। पादरी बनने के लिए असंख्य विद्यार्थियों को भर्ती किया जाता है, मगर उनमें से बहुत कम को पसन्द किया जाता है।’’ कथा लेखन में सर्जनात्मकता की जयमाला लेखक की सभी रचनाओं को शाश्वत सुरभि के साथ प्राप्त नहीं होती है। असूर्यलोक में कथागुम्फन लेखक बना रहे कोये-जैसा है। ‘‘तब वह नगर सन्ध्या बेला में डूब रहे सूरज के समान लग रहा था।’’—इस वाक्य से आरम्भ होकर भद्रशंकर, निगमशंकर, तिलक और पर्जन्य तक पहुँचकर चार पीढ़ियों के साठ से अधिक वर्षों की समयावधि में व्यस्त होकर ‘‘जगन्नाथ के रथ के पहियों से किचुड़-किचुड़ आवाज़ निकली। रथ आगे बढ़ा बढ़ता ही रहा’’ जैसे वाक्य के साथ पराकाष्ठा के बिन्दु तक पहुँच रही इस कृति को पूरा पढ़ लेने के बाद यह प्रस्तावना लिखने वाले को विश्वास हो गया कि जिन लोगों का आह्वान किया है और इने-गिने व्यक्तियों को चुना गया है उनमें भगवती कुमार शर्मा अवश्य हैं।
भगवती कुमार शर्मा की सृजनयात्रा का आरम्भ कवि रूप में हुआ, साथ ही वे कहानी, उपन्यास और निबन्ध की विधाओं में भी आगे बढ़ते रहे हैं। एक पत्रकार के रूप में घटना को बाहर से देखना और कवि के रूप में उसे भीतर से अनुभव करना—यह वरदान के साथ ही अभिशाप भी है। इस दृष्टि से भगवतीभाई झवेरचंद मेघाणी या चुनीलाल माड़िया की परम्परा निभा रहे हैं। फिर भी उनकी निजी मुद्रा उभरती है।
असूर्यलोक में भगवतीकुमार अपने अनेक बार दुहराये गये विषय को फिर से ले आते हैं। अनाधिकार—जैसी कहानियों में, समयद्वीप—जैसे उपन्यासों में दिखाये गये संघर्षों की कुछ लकीरें यहाँ भी पायी जाती हैं : विषय का पुनरावर्तन है, लेकिन यहाँ संघर्ष बिलकुल ही भिन्न प्रकार का है। लेकिन जैसे फ्रांसीसी लेखक सेलान ने कहा है :’’
We shall never beat peace, until everything has been said, once for all times.’’
भगवतीकुमार जो कहना चाहते हैं, उसके लिए कहानी या लघु उपन्यास का ढाँचा छोटा पड़ रहा था। सशक्त संरचनावली कृति में कभी-न-कभी इसे प्रकट होना ही था। उत्तम कलाकृति के प्रथम प्रयोग के पहले ग्रांड रिहर्सल में इसे विविध अंशों में उभारना संभव हुआ था। पहले की कृतियों में समय और स्थल के परिणाम भिन्न थे। असूर्यलोक में समय और स्थल के परिणाम सूक्ष्म रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। मध्यकालीन युग के पहले से यूरोप के साहित्य में ‘सागा’’’ (अनेक पीढ़ियों तक फैलती इतिहासगाथा) लिखने की प्रणाली थी। हमारे यहाँ रघुवंशम् भी एक ‘‘सागा’’ ही है। गाल्सवर्दी ने अपनी कृति फोरसाइट सागा द्वारा इस कथारूप को सामाजिक सन्दर्भ दिया है। जैसा कि पश्चिम के एक समीक्षक ने कहा है, क्या कब घटा है, इसकी बात कहना आरम्भ करें, तब वह इतिहास होता है। क्यों और कैसे वह घटा, यह कहने लगे, तब उपन्यास बन जाता है। भगवतीकुमार ने सागा की इतिहास शैली अपनाकर उसे कथा के रूप में कालस्वरूप दे दिया है।
शीर्षक से ही कृति का रस घुटने लगता है। पहले ही प्रकरण में ईशावास्य के ‘असूर्या नाम ते लोका’ के साथ उलझता नहीं है। उस श्लोक में ‘असूर्य’ और ‘लोक’ दोनों शब्द हैं लेकिन यह असूर्य लोक वह नहीं है, जो भगवती कुमार को अभिप्रेत है। असूर्यलोक की पहचान तो आरम्भ के पृष्ठों में नगर के वर्णन में ही मिल जाती है। ‘‘धुएँ की उन छोटी, नीची दीवारों को फांदकर डगमग गुज़र रही सँकरी सड़कें, ऊबड़-खाबड़ लेकिन ख़ामोश सड़कें...सर्दियों की शाम जैसी या लालटेन के धब्बेदार गोले, जैसी धुँधली धब्ब आँखें, धुँधले अक्षरों में लिखा गया डॉ. श्रीधर तांजोरकर (के नाम) का बोर्ड नगर की कुहासे भरी छवि में पूर्णतया एकरूप हो गया था, उन क्षणों पर वर्षों के उपले-कंडों की राख जम गयी थी, जगमगाते हुए क्षणों में काले भालू के लहू के मोटे लट्ठ रेले की तरह अचानक ही अँधेरा छा गया, भरी दुपहर में भी दिशाएँ मैली धुँधली। अम्बा माँ ने पोस्टकार्ड बढ़ाया। निगमशंकर ने टटोलकर उसे हाथ में लिया, आँखों के सामने रखा, लेकिन अक्षर सारे अंतर्धान !’’ ‘‘तुम अपनी पढ़ाई भूल गए या फिर तुम्हारी आँखों में कुँए खोद दिये गये हैं ?’’ ‘‘टटोलना, यही क्या जीवन का पर्याय बना रहेगा ?’’ ‘‘सूबह की धूप फैलते-फैलते ही सिमट गयी।’’ यहाँ तक अन्धकार आवृत होने के कारण अंध असुरों के लोक का सन्दर्भ रहता है, परंतु सोलह साल की उम्र में जिसने अचानक ही आँखें खोल दी थीं, उस निगमशंकर से पण्डित विनोदानन्द झा पूछते हैं, ‘‘बन्धु, तुम पढ़ने के लिए काशी चलोगे ?’’ भगवती कुमार आगे लिखते हैं : ‘‘काशी ? निगमशंकर रोम-रोम से आन्दोलित हो उठे। उन्हें ऐसा लगा कि उनका अनधत्व दूर हो गया था और किसी मन्दिर के गुम्बद के स्वर्णकलश जैसा प्रकाश चारों ओर फैल गया था। मानो वे पंडित विनोदानन्द झा का चेहरा देख सकते थे और पोथियों में सामवेद के मंत्रों के अक्षर और स्वर भी दिखायी देने लगे थे। कुछ समय से माँ का जो मुख देख नहीं पा रहे थे, वह भी (आँखों के सामने) झिलमिला उठा और अम्बा माँ ने भरी दोपहरी में पढ़कर सुनाने को जो पत्र दिया था, वह भी पुनः साकार हो उठा और अब तो उस पत्र का हर अक्षर....’’ यहीं इस अंतिम वाक्य में आगे के छह सौ पृष्ठों में भगवतीभाई जिसकी बात करने जा रहे हैं उस ‘असूर्यलोक’ का प्रथम दर्शन होता है।
उपर्युक्त उद्धरणों में सहज रूप से ही लेखक की शैली के कुछ उदाहरण मिल गये हैं। भगवतीभाई की इसके पहले की कृतियों की भाषा के साथ इनकी तुलना करनी चाहिए। डब्ल्यू.बी. यीट्स अपने एक नाटक की प्रस्तावन में कहते हैं : ‘‘जैसे मैंने अपने वाक्य-विन्यास, कारक प्रक्रिया को बदला, वैसे ही अपनी प्रज्ञा को भी नया रूप दिया। (As I altered my syntax, I altered my Intellect) भगवतीकुमार अपनी कारक प्रक्रिया को बदलते हैं और प्रथम प्रकरण से ही इनकी प्रतीति हो जाती है। जब लेखक एक ही ढंग से लिखता रहता है, एक ही ढंग से पात्रों को ढालता है, तब उसमें वैविध्य होने पर भी गति नहीं होती है। यहाँ हम प्रज्ञा को, सर्जकता को नया रूप देने वाली कारक प्रक्रिया के साक्षी बनते हैं।
भगवती कुमार यहाँ अपनी वैविध्यपूर्ण विरासत को निरूपित करते हैं। जन्म से और कर्म से ब्राह्मण होने के कारण वे वैयक्तिक ढंग से बड़े हुए। एकओर आसपास के वातावरण आदि से आनेवाली विरासत है, तो दूसरी ओर वह विरासत है जो भारतीय संस्कृति के मूल्यों को लेकर टिकी हुई है। यो दोनों विरासतें उनकी सर्जकता के बिन्दु में एक रूप हो जाती हैं। उनके पास वे सत्य हैं जो अभिव्यक्त होने के लिये व्याकुल हैं। पहले भी अपूर्ण रूप से वे सत्य अभिव्यक्त होते रहे हैं। अब वे सभी सत्य उनके द्वारा समग्र रूप से प्रकट होने के लिये अधीर हो रहे हैं। यहाँ यथार्थ का निरूपण नहीं है, अपितु अनुभव लोक की प्रतिष्ठा है। यह अनुभव लोक यथार्थ पर आधारित है। कथासाहित्य में निहित सत्य जीवन के सत्य की अपेक्षा अधिक यथार्थपूर्ण होता है। फिर एक बार उपन्यास के स्वरुप के विषय में गंभीर रूप से चिंतन करने वाले राइट मोरिस का स्मरण हो आता है। वे कहते हैं : ‘‘हम यथार्थ के आधार पर जीने की कोशिश करते हैं, परन्तु जीने का उद्यम तो कथा साहित्य में ही करते हैं। केवल कथालोक ही जीवन के यथार्थ को पूर्णरूप से अपने में समा लेता है।’’
असूर्यलोक उपन्यास है। ‘पर्जन्य तिलक त्रिवेदी’ या ‘तिलक निगमशंकर त्रिवेदी’ या ‘निगमशंकर भद्रशंकर त्रिवेदी’—ये नाम किसी नगरपालिका या शाला के दफ़्तर में दर्ज नहीं हुए होंगे। अगरचे सत्य कभी कथालोक से अधिक चौंका दे, इस तरह यथार्थ से स्पर्धा करता है। (वैसे यह हुआ भी हो, तो भी वह पर्जन्य, तिलक या निगमशंकर भिन्न ही होंगे।) फिर भी जब इस उपन्यास को अंत तक पढ़ लेते हैं, तो वासनामय जीवन के कीट के रूप में अंतिम साँस ले रहे भद्रशंकर, ज्ञान में और भागीरथी की आँखों के दीये निहार रहे निगमशंकर, ज़िन्दगीभर कहीं आँखों में कुएँ तो नहीं बने रहेंगे—इस भय के साथ जी रहा तिलक, एक क्षण में विवाह की पूर्व-रात्रि में अपना सर्वस्व तिलक के चरणों में समर्पित करनेवाली धरती तथा देव के प्रसाद के रूप में संसार को निभा रही सत्या, ईक्षा, गोरधन सेठ और सजल, सत्या के साथ पुनर्मिलन के समय ही तिलक की आँखों की दृष्टि का विलीन हो जाना और सत्या के नगर में आगमन के साथ ही सजल का प्राण त्यागना—ये घटनाएँ और सजल के प्राणत्याग के बावजूद उसके कार्य को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प कर रहा कृतार्थ और तिलक के कार्य-क्षेत्र के मधुवन में सत्या के सामने चलकर माँगे हुए तथा अपने भीतर रोपे हुए और अपने रेगिस्तान में जतन से बड़े किये हुए परिजात-जैसा पर्जन्य तिलक के मधुवन में महक फैलाना चाहें, तब सत्या के अल्पाधिक सौभाग्य पर सामाजिक सम्मति की मुहर लगा रहे गोरधन सेठ और उपन्यास के कुछ विकट क्षणों में ही उपस्थित रहनेवाले कृष्णजी...(महाभारत में कृष्ण द्वैपायन कर्ता भी हैं और कथा के पात्र भी, किंतु यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि कहीं-कहीं सर्जक स्वयं कर्ता और पात्र के रूप में तो नहीं आ गये हैं ?) आदि पात्र मानो चिरकाल से पहचाने हुए हों, वैसे मन में बस जाते हैं।
अन्य पात्रों के बारे में भी कहा जा सकता है। पर इतने पात्रों की भी पूरी पहचान कहाँ दे पाया हूँ ?
भगवती कुमार ने इन पात्रों को जीवन का परिमाण दिया है। कहते हैं कि सर्जक कोई समस्या पैदा कर दे और उसका हल भी ला दे, इसके साथ ही वह इस धरती पर के जीवनसत्य का दर्शन कराता है। भगवतीकुमार ने असूर्यलोक के तेजोमय रूप को प्रकट करने वाले कुछ जगमगाते पात्रों का सृजन किया है। उन्हें केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी आकार दिया है। जेम्स जॉयस ने कहा है;
‘‘Any man of real individuality tries to know and to understand what is happening, even in himself, as he goes along.’’
भगवतीभाई ने सृजन पथ पर अपनी यात्रा आँखें खुली रखकर की है। उस यात्रा में उन्हें जो पात्र मिल गये, वे इन छह सौ पृष्ठों का नेत्र प्रवास पूरा होने तक केवल पात्र नहीं रहते हैं। मैं आपको अचूक पहचान दे सकता हूं। यह तिलक, इससे आप मिले नहीं हैं क्या ? स्थूल महत्त्वाकांक्षा को त्यागकर केवल ग्रंथालय में प्रज्ञा के बीच ही रहना जिसे पसन्द था, वह अनूठा युवक—और यह सत्या, चंचल और अनर्गल प्रेम करने वाली, दुनिया के प्रति बेपरवाह, फिर भी परिस्थितियों की परिसीमा को अखण्डित रखकर जीनेवाली आसाधारण नारी...हाँ, इन सभी पात्रों को मैं पहचानता हूँ। आपकी मैं उनसे पहचान कराता हूँ; बहुत कुछ कह सकता हूँ। पर अच्छे लोगों से परिचय कराने के बाद से परिचय करानेवाले बहुत देर तक रुकते नहीं हैं। आप उनसे मिल लें इसके बाद आपका अगर मुझसे मिलना होगा तो आप कहेंगे; ‘‘ये पात्र तो जैसा आपने कहा था, हमसे भी अधिक जीवंत निकले !’’ केवड़े की सुगंध की भाँति प्रवेश कर रही निगमशंकर की नयी माँ से लेकर उपन्यास पराकाष्ठा के बिन्दु तक पहुँचता है, तब तक आनेवाले सभी पात्रों के बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं चाहे कितना भी कहूँ, इन पात्रों से मिलने के बाद आप मुझसे कहेंगे : ‘‘अरे, इन सबके बारे में आपने कुछ कहा ही कहाँ है ?’’
भगवती भाई,
आपसे दो बातें कहनी हैं। मुझे विश्वास है कि उपन्यास पढ़ लेने के बाद अनेक पाठक इसके नीचे अपने हस्ताक्षर करने को प्रेरित होंगे। चित्त को प्रसन्न कर दे, ऐसी सशक्त रचना देने के लिए अपने शब्दों द्वारा मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उत्तम सृजन करने वाले सर्जक के प्रति कृतज्ञता का सूर्य हृदय में जगमगाता ही रहता है।
इस कृति ने मेरा भी निर्माण किया है
हालाँकि इस उपन्यास का धुँधला-सा विचार तंतु 1984 के दिसम्बर या 1985 के जनवरी में पहली बार मेरे मन में प्रकट हुआ था, किंतु वास्तव में असूर्यलोक का बीज लेकर ही मैं पैदा हुआ था। कोई दस साल की उम्र में आँखों पर पहली बार चश्मा लगा, तब से अन्तर्मन में जो बीज बोया गया होगा, उसे करीब साढ़े चार दशकों के बाद इस उपन्यास में वृक्ष का रूप में प्राप्त हुआ है। 1985 में कई महीने में असूर्यलोक का लेखन आरम्भ करके कोई दो महीने में उसे पूरा कर दिया, तब मैं आनन्दविभोर हो गया। जब उसका पुनर्लेखन करना शुरू किया तो हर शब्द मुझे चुनौती देने लगा। फिर भी दो-तिहाई कार्य तो पूरा कर ही दिया। फिर गंभीर बीमारी के कारण तीन महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ा। निष्क्रियता के उस कालखण्ड में उपन्यास और कथालेखन का भीतरी लय टूट गई। पात्र, घटनाएँ, निरूपण—इनके बारे में मन में अनेक प्रश्न उठे। अनेक नये बिन्दु भी सूझ गये। स्वास्थ्य ठीक होने पर पांडुलिपि को फिर से हाथ में ले लिया। लेकिन मन दृढ़तापूर्वक इंकार करने लगा—यह नहीं चल सकता।’’ ‘और पुनश्च हरिओम’ करके असूर्यलोक तीसरी बार आरम्भ किया जो 1986 के नवम्बर तक पूरा किया। केवल यह हुआ कि पहले और तीसरी बार के लेखन के बीच उपन्यास का हृदय तो टिका रहा, परंतु इसे छोड़कर पूरा ढाँचा ही बदल गया। इस उपन्यास की रचना—प्रक्रिया में मेरी धृति की बड़ी भारी कसौटी हो गई। साथ ही इस उपन्यास ने मेरे हृदय की श्रद्धा का भी पुनर्निर्माण किया। इसे लिखने के पहले मैं जो था, वह काफी हद तक इसे लिख लेने के बाद नहीं रह गया होऊँगा।
आसूर्यलोक को बम्बई के प्रसिद्ध साप्ताहिक जन्म-भूमि में धारावाहिक रूप में प्रकट होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। इसका सारा यश उस पत्र के सम्पादक और विख्यात कवि और साहित्यकार श्री हरीन्द्र दवे को है। उन्होंने तथा उनके सहकारी श्री हिम्मत भाई मेहता, श्रीत्र्यंबक महेता, प्रताप के संपादक श्री जगदीश शाह, तरु बहन कजीरिया, भाई विनीत शुक्ल और अन्य व्यक्तियों ने इस कृति के प्रति सद्भाव व्यक्त किया। उन सबका मैं ऋणी हूँ। हरीन्द्र भाई ने जन्मभूमि-प्रवासी में असूर्यलोक के समापन के समय अत्यंत उत्साह भरे शब्द लिखे और बाद में इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखने का मेरा अनुरोध भी माना। उनका यह बन्धुकृत्य मेरे जीवन की एक मधुरतम स्मृति बनकर रहेगा। उनके ऋण-स्वीकार के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं।
असूर्यलोक के धारावाहिक प्रकाशन को पाठकों का जो अपार प्रेम प्राप्त हुआ है, यह भी मुझे धन्य करने वाला अनुभव था। आदरणीय श्री उमाशंकर जोशी, श्रीमती कुन्दनिका कापडीआ, श्री शिवकुमार जोशी, श्री दिलीप राणपुरा, श्री जयंतीलाल महेता, श्री प्रकाश न. शाह आदि सारस्वतों ने इस कृति में रुचि लेकर मुझे स्नेहसिक्त किया, इसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ।
लंदन के वयोवृद्ध समीक्षक लेखक माननीय श्री भानुशंकर ओ. व्यास ने तो असूर्यलोक को अपनी ही कृति मानकर लंदन से उस पर वात्सल्य की वर्षा की। इस पुस्तक के सन्दर्भ में उनके लिखे हुए पत्रों की एक स्वतंत्र पुस्तक बनाई जा सकती है। इन पत्रों का एकाध अंश इस पुस्तक में शामिल कर दिया है। मेरे लिए भानुभाई का सौजन्य अविस्मरणीय है। दुर्भाग्य से वे इस पुस्तक को देख पायें, इसके पहले उनका दु:खद निधन हो गया।
मुझे बार-बार ऐसा लगता है कि किसी अगम्य तत्व ने मुझे इस उपन्यास को लिखने के लिए प्रेरित किया है। अनेक व्यवधानों के होते हुए भी यह उपन्यास परिपूर्ण हो सका, इसके लिए मुझे परम तत्व के संचरण का विनीत भाव से आभारी होना चाहिए विख्यात अध्यात्मचिंतक डॉ. कांतिलाल कालाणी के आशीर्वाद इस कृति के सृजन के दरम्यान मुझे प्राप्त होते ही रहे हैं। ‘‘आप जब उपन्यास लिख रहे थे, तब मैं आपके साथ ही था।’ उनके ये शब्द मेरे जीवन की अनमोल संपत्ति हैं। अपने संतोष, प्रेरणा और अवतरणों के विषय में मैंने डॉ. कलाड़ी का तथा कवि श्री मकरन्द दवे के ग्रन्थ विष्णु सहस्रनाम : आंतरप्रवेश का आधार लिया है। इन दोनों महानुभवों के आगे मैं प्रमाणित करता हूँ ।
इसके अतिरिक्त असूर्यलोक के नामकरण में सहायरूप बननेवाले भाई कपिल देव शुक्ल, इस उपन्यास में आने वाली नेत्ररोग से सम्बन्धित चर्चा में अधिकृत जानकारी देनेवाले सूरत के मशहूर नेत्रचिकित्सक डा. के.के. देसाई, ज्यां पाल सार्त्र के अवतरणों के लिए उनकी साक्षात्कार की पुस्तिका के अनुवादक आदरणीय श्रीगुलाबदास ब्रोकर, मुझे यह उपन्यास लिखने की सुविधा प्रदान करने वाले मेरे मित्र श्रीनानूभाई नायक, जनक नायक और सौभाग्यवती जयश्री नायक, इस कृति की प्रतियोंके जतन में सहायक होनेवाले प्रो. मुकेश कॉन्ट्रेक्टर, श्री दिनेश अनाजवाला, असूर्यलोक के लेखन में आदि से अंत तक मेरे साथ रहने वाली मेरी पुत्री चि. रीना, मेरे सभी स्वजन सौ. ज्योति, चि.मेहूला, सौ. झरना, चि. रुचिरा, श्री चंद्रकांत भाई पांड्या, मेरे मिक्त्र मनहर भाई चौक्सी, नयन देसाई रवीन्द्र पारेख, बकुलेस देशाई, और प्रसिद्ध समीक्षक श्री कृष्णवीर दीक्षित—इन सबके प्रति मैं हृदयपूर्वक आभार प्रकट करता हूँ। असूर्यलोक में निगमशंकर को जो अंधत्व आता है, उस घटना का प्रज्ञाचक्षु पंडित सुखलाल जी के जीवन की एक ऐसी घटना के आधार पर निरूपण किया है। निगमशंकर के ग्रंथ भंडार का बाढ़ में नष्ट हो जाना—इससे मिलती-जुलती घटना बरसों पहले श्री कांति भडिया के एक सुंदर नाटक में देखी थी, ऐसा कुछ स्मरण है।
ऊर्ध्वमूल के लेखन-प्रकाशन के बहुत ही लम्बे समय के बाद असूर्यलोक उपन्यास आया है। ऊर्ध्वमूल को पाठकों-समीक्षकों का विपुल प्रेम प्राप्त हुआ था। असूर्यलोक के सम्बन्ध में इसका पुनरावर्तन होगा तो मेरा सृजनश्रम सार्थक हो जायेगा। सरस्वतीचंद्र जैसे हमारे ग्रंथ मणि के प्रकाशन की और कन्हैयालाल मुंशी जैसे हमारे समर्थ उपन्यासकार की जन्म शताब्दी के वर्ष में असूर्यलोक का प्रकाशन हो रहा है, उस सुखद संयोग से धन्यता का अनुभव करता हूँ। मुझे यह निखालिस भाव से कहना चाहिए कि असूर्यलोक मैंने लिखा है, इससे अधिक तो इस कृति ने साथ-ही-साथ मेरे भीतर लक्ष-लक्ष में अक्षर अंकित किये हैं। सर्जक कृति का निर्माण करता है, कृति भी सर्जक का आंतरिक निर्माण कर सकती है, इस रचना की सृजन-यात्रा से मुझे यह अनुभव हुआ है, इस लीला के नियंता ऐसे परम तत्व के चरणों में सिर झुका कर यह कृति आप सबको सादर समर्पित करता हूँ।
एक
यह नगर उस समय सन्ध्याकाल के डूबते हुए सूरज के समान था : धुँधला, मितभाषी, नम, उदास। बाद में कितने ही ढंग से उसका विस्तार हुआ है। वह बहक गया है। उसका कलेजा सिकुड़ गया है। अन्ध गति के कारण शहर सतत और बेतहाशा हाँफता है। बत्तियों की उन्मादभरी जगमगाहट से उसकी दृष्टि धुँधली होती जा रही है।
कोई साठ साल पहले इस नगर की धूलभरी गलियों में और घरों में, छप्पर पर के कच्चे खपरैलों पर बरस रहा पानी कितने ही दिनों तक भीगी महक फैलाता रहता था। गलियों के वृक्षों से पत्ते और पानी की बूँदें गिरती रहती थीं। छोटे कच्चे मकानों में मँडरा रहा धुआँ आकाश की निस्सीमता में घुल जाता था। खाना पका रही स्त्रियों की चूल्हे में मारी हुई फूँक और विद्वान ब्राह्मणों के अग्निहोत्र दोनों उस धुएँ के उद्गम स्थान होते थे। उन धूम्रवलयों में स्त्रियों के गीत और विश्वास वेदपाठियों के मंत्रोच्चार, श्रीमंतो की ऊँची मंजिलों में बज रहे ग्रामोंफोन के रिकार्डों में से लहराते नाटकों के गानों के सुर, पहाड़े रट रहे लड़कों के विलम्बित स्वर, मौखिक हिसाब पूछ रहे बुजुर्गों की हाँक, शाला के शिक्षकों के फुट्टे की चमचमाहट, लालटेन और एरंड के तेल के दीये के उजास की धुँधली आड़ी-तिरछी रेखाएँ—सब कुछ शहर के खुले, प्रदूषित आकाश में मंडराता रहता था। नगर के मिडल स्कूल में और हाईस्कूल में कम्पाउन्ड में बॉयस्काउट कैम्प-फायर जलाते थे और शहर के एक मात्र आर्ट्स-साइंस कॉलेज के रोबदार प्रिंसिपल के ऐंठते होंठों के बीच दबी काली पाइप में से झिलमिल हो रही तम्बाकू की बू से भरी धूम्र रेखा—उन दोनों के बीच कुछ संगति थी।
धुएँ की उन छोटी, नीची दीवारों को लाँघकर डगमग गुज़र रही शहर की सँकरी, असमतल और सूनी सड़कों पर से आँखों के स्थान पर केवल दो खड्डे टिकाए हुए ज़िन्दा लोग भी किसी की उँगली तक पकड़े बिना संदेशवाहक कबूतर की भाँति आर-आर चले जा सकते थे, ऐसा उस समय का नगर था—स्वस्थ, सुख-चैन देनेवाला नगर। बाद में तो।
जाड़ों की शाम-जैसी या लालटेन के धब्बेदार गोले-जैसी धुँधली-धुँधली आँखों की चिकित्सा के लिए शहर सबसे पहला क्लीनिक डॉ. श्रीधर तांजोरकर का खुला था। धुँधले अक्षरों में लिखा हुआ उनके नाम का बोर्ड नगर की कोहरेदार छवि में बिल्कुल एकरूप हो गया था। और इसे तो निगमशंकर भद्रशंकर त्रिवेदी जैसे पंडित भी नहीं पढ़ सकते थे। किंतु....
निगमशंकर को ठीक याद था वह क्षण—हालाँकि उस पर 52 वर्षों के उपलों-कंडों की राख जम गयी थी; फिर भी उनके मनः चक्षु के आगे वह क्षण घुँघची की तरह चमक रहा था। दूर के शैशव से शायद इतना ही उनके लिए बचा रह गया था, जिसे ओजस्वी कहा जा सके।
शहर की पाठशाला में सुबह के सत्र में संस्कृत का अध्ययन करके लौट रहे कोई सोलह साल के लम्बे, गोरे, सशक्त निगमशंकर के गंजे सिर पर लम्बी शिखा और कन्धे पर ओढ़ा हुआ केसरिया रंग का उपवस्त्र, दोनों गरम हवा के फर्राटे में फरफरा रहे थे। मध्याह्न का सूर्य दस नहीं ग्यारह दिशाओं में फैलते हुए गोनी भर-भरकर धूप उँड़ेल रहा था। ऐसे जगमगाते क्षण में काले भालू के लहू के मोटे लट्ठ रेले की तरह अन्धकार अचानक ही फैल गया। आँखों के सामने जाने कैसा पर्दा आ गया। इसका रंग काला था, निगमशंकर को इतना समझ में आ गया। यह दुःस्वप्न होगा या पाँव वर्तुल में पड़ जाने का क्षणिक परिणाम होगा, ऐसा मानकर वे आगे बढ़े। लेकिन दोनों पाँव मानो गोबर की लोंदे हो गये। शरीर में ज्वर और दर्द का अनुभव हुआ। जल्दी घर पहुँचने की अधीरता बबूल की कँटीली डाली की तरह उनके जी को नोचने लगी। घर में जितना संभव हो कम और पाठशाला में अधिक समय बितानेवाले निगमशंकार को लगा कि शरीर बिखरने लगा था और भारी दोपहर में भी दिशाएँ मटमैली...
ग्रहण के समय साँप दीख जाये, वैसे वृद्ध अम्बा माँ टकरा गयी और निगमशंकर के लिए आवाज़ से पहचाने जाने वाला प्रथम पात्र बन गयीं। वे दूर की बुआ लगती थीं। उन्होंने अगर पुकारा न होता तो निगमशंकर ने उन्हें पहचाना नहीं होता। लेकिन माँ जी ने भतीजे को देख लिया था : ‘‘अच्छा हुआ तुम मिल गये, निगम ! बम्बई से मुन्ना की चिट्ठी आयी है। इसे पढ़ाने के लिये मैं तुम्हारे पास आ रही थी। मुझ मुई के लिए तो काले अक्षर भैंस बराबर हैं। तुम पढ़ दो न बेटे ! तुम तो पढ़े लिखे हो...’’ कहकर अम्बा माँ ने पोस्ट कार्ड आगे बढ़ाया। निगमशंकर ने टटोलकर कार्ड अपने हाथ में ले लिया और आँखों के सामने पकड़कर रखा, लेकिन अक्षर सभी अंतर्धान ! उँगलियों के पोरों को पोस्टकार्ड का स्पर्श हो रहा था बस। वेदसंहिता की पोथियाँ और सिद्धांतकौमुदी के पृष्ठों को उँगलियों से पकड़कर जल्दी से पढ़ने की आदी बन चुकी निगमशंकर की आँखों के लिए यह छोटी-सी चिट्ठी पढ़ पाना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने आँखों की लगाम तंग की। व्यर्थ ! ‘‘क्यों बेटे, आज ऐसा क्यों ? जो पढ़ना सीखे हो उसे भूल चुके हो या फिर तुम्हारी आँखों में कुएँ खोद दिये गये हैं ?’’ माँ जी ने अचरज के साथ कहा। ‘‘हाँ, बुआ जी, कुछ ऐसा ही लग रहा है...’’ बोलते-बोलते निगमंकर का स्वर रुँधने लगा। लड़खड़ाते हुए, गिरते-पड़ते और ठोंकरे खाते-खाते मुश्किल से घर की दिशा में मुड़े। ‘‘आओ, बेटे मैं तुम्हें घर पहुँचा देती हूँ।’’ अपने पीछे इस तरह सुनायी दे रही माँ जी की पुकार उन्होंने अनसुनी कर दी। कब तक कोई घर पहुँचाने आयेगा ? टटोलना—क्या जीवन का अब यही पर्याय बनकर रहेगा ?
कोई साठ साल पहले इस नगर की धूलभरी गलियों में और घरों में, छप्पर पर के कच्चे खपरैलों पर बरस रहा पानी कितने ही दिनों तक भीगी महक फैलाता रहता था। गलियों के वृक्षों से पत्ते और पानी की बूँदें गिरती रहती थीं। छोटे कच्चे मकानों में मँडरा रहा धुआँ आकाश की निस्सीमता में घुल जाता था। खाना पका रही स्त्रियों की चूल्हे में मारी हुई फूँक और विद्वान ब्राह्मणों के अग्निहोत्र दोनों उस धुएँ के उद्गम स्थान होते थे। उन धूम्रवलयों में स्त्रियों के गीत और विश्वास वेदपाठियों के मंत्रोच्चार, श्रीमंतो की ऊँची मंजिलों में बज रहे ग्रामोंफोन के रिकार्डों में से लहराते नाटकों के गानों के सुर, पहाड़े रट रहे लड़कों के विलम्बित स्वर, मौखिक हिसाब पूछ रहे बुजुर्गों की हाँक, शाला के शिक्षकों के फुट्टे की चमचमाहट, लालटेन और एरंड के तेल के दीये के उजास की धुँधली आड़ी-तिरछी रेखाएँ—सब कुछ शहर के खुले, प्रदूषित आकाश में मंडराता रहता था। नगर के मिडल स्कूल में और हाईस्कूल में कम्पाउन्ड में बॉयस्काउट कैम्प-फायर जलाते थे और शहर के एक मात्र आर्ट्स-साइंस कॉलेज के रोबदार प्रिंसिपल के ऐंठते होंठों के बीच दबी काली पाइप में से झिलमिल हो रही तम्बाकू की बू से भरी धूम्र रेखा—उन दोनों के बीच कुछ संगति थी।
धुएँ की उन छोटी, नीची दीवारों को लाँघकर डगमग गुज़र रही शहर की सँकरी, असमतल और सूनी सड़कों पर से आँखों के स्थान पर केवल दो खड्डे टिकाए हुए ज़िन्दा लोग भी किसी की उँगली तक पकड़े बिना संदेशवाहक कबूतर की भाँति आर-आर चले जा सकते थे, ऐसा उस समय का नगर था—स्वस्थ, सुख-चैन देनेवाला नगर। बाद में तो।
जाड़ों की शाम-जैसी या लालटेन के धब्बेदार गोले-जैसी धुँधली-धुँधली आँखों की चिकित्सा के लिए शहर सबसे पहला क्लीनिक डॉ. श्रीधर तांजोरकर का खुला था। धुँधले अक्षरों में लिखा हुआ उनके नाम का बोर्ड नगर की कोहरेदार छवि में बिल्कुल एकरूप हो गया था। और इसे तो निगमशंकर भद्रशंकर त्रिवेदी जैसे पंडित भी नहीं पढ़ सकते थे। किंतु....
निगमशंकर को ठीक याद था वह क्षण—हालाँकि उस पर 52 वर्षों के उपलों-कंडों की राख जम गयी थी; फिर भी उनके मनः चक्षु के आगे वह क्षण घुँघची की तरह चमक रहा था। दूर के शैशव से शायद इतना ही उनके लिए बचा रह गया था, जिसे ओजस्वी कहा जा सके।
शहर की पाठशाला में सुबह के सत्र में संस्कृत का अध्ययन करके लौट रहे कोई सोलह साल के लम्बे, गोरे, सशक्त निगमशंकर के गंजे सिर पर लम्बी शिखा और कन्धे पर ओढ़ा हुआ केसरिया रंग का उपवस्त्र, दोनों गरम हवा के फर्राटे में फरफरा रहे थे। मध्याह्न का सूर्य दस नहीं ग्यारह दिशाओं में फैलते हुए गोनी भर-भरकर धूप उँड़ेल रहा था। ऐसे जगमगाते क्षण में काले भालू के लहू के मोटे लट्ठ रेले की तरह अन्धकार अचानक ही फैल गया। आँखों के सामने जाने कैसा पर्दा आ गया। इसका रंग काला था, निगमशंकर को इतना समझ में आ गया। यह दुःस्वप्न होगा या पाँव वर्तुल में पड़ जाने का क्षणिक परिणाम होगा, ऐसा मानकर वे आगे बढ़े। लेकिन दोनों पाँव मानो गोबर की लोंदे हो गये। शरीर में ज्वर और दर्द का अनुभव हुआ। जल्दी घर पहुँचने की अधीरता बबूल की कँटीली डाली की तरह उनके जी को नोचने लगी। घर में जितना संभव हो कम और पाठशाला में अधिक समय बितानेवाले निगमशंकार को लगा कि शरीर बिखरने लगा था और भारी दोपहर में भी दिशाएँ मटमैली...
ग्रहण के समय साँप दीख जाये, वैसे वृद्ध अम्बा माँ टकरा गयी और निगमशंकर के लिए आवाज़ से पहचाने जाने वाला प्रथम पात्र बन गयीं। वे दूर की बुआ लगती थीं। उन्होंने अगर पुकारा न होता तो निगमशंकर ने उन्हें पहचाना नहीं होता। लेकिन माँ जी ने भतीजे को देख लिया था : ‘‘अच्छा हुआ तुम मिल गये, निगम ! बम्बई से मुन्ना की चिट्ठी आयी है। इसे पढ़ाने के लिये मैं तुम्हारे पास आ रही थी। मुझ मुई के लिए तो काले अक्षर भैंस बराबर हैं। तुम पढ़ दो न बेटे ! तुम तो पढ़े लिखे हो...’’ कहकर अम्बा माँ ने पोस्ट कार्ड आगे बढ़ाया। निगमशंकर ने टटोलकर कार्ड अपने हाथ में ले लिया और आँखों के सामने पकड़कर रखा, लेकिन अक्षर सभी अंतर्धान ! उँगलियों के पोरों को पोस्टकार्ड का स्पर्श हो रहा था बस। वेदसंहिता की पोथियाँ और सिद्धांतकौमुदी के पृष्ठों को उँगलियों से पकड़कर जल्दी से पढ़ने की आदी बन चुकी निगमशंकर की आँखों के लिए यह छोटी-सी चिट्ठी पढ़ पाना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने आँखों की लगाम तंग की। व्यर्थ ! ‘‘क्यों बेटे, आज ऐसा क्यों ? जो पढ़ना सीखे हो उसे भूल चुके हो या फिर तुम्हारी आँखों में कुएँ खोद दिये गये हैं ?’’ माँ जी ने अचरज के साथ कहा। ‘‘हाँ, बुआ जी, कुछ ऐसा ही लग रहा है...’’ बोलते-बोलते निगमंकर का स्वर रुँधने लगा। लड़खड़ाते हुए, गिरते-पड़ते और ठोंकरे खाते-खाते मुश्किल से घर की दिशा में मुड़े। ‘‘आओ, बेटे मैं तुम्हें घर पहुँचा देती हूँ।’’ अपने पीछे इस तरह सुनायी दे रही माँ जी की पुकार उन्होंने अनसुनी कर दी। कब तक कोई घर पहुँचाने आयेगा ? टटोलना—क्या जीवन का अब यही पर्याय बनकर रहेगा ?
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book