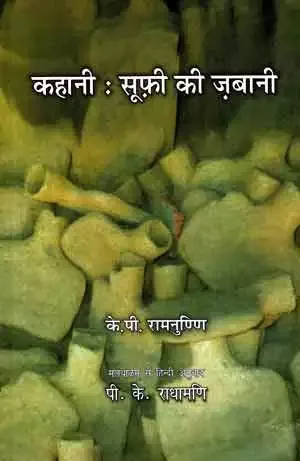|
उपन्यास >> कहानी : सूफी की जबानी कहानी : सूफी की जबानीपी.के.राधामणि
|
321 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत उपन्यास कहानीः सूफी की ज़बानी केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा प्रतिष्ठित इडश्शेरी अवार्ड से सम्मानित मलयालम उपन्यास सूफी परंज कथा का हिन्दी अनुवाद है
Kahani Sufi Ki Jabani
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्रस्तुत उपन्यास कहानीः सूफी की ज़बानी केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा प्रतिष्ठित इडश्शेरी अवार्ड से सम्मानित मलयालम उपन्यास सूफी परंज कथा का हिन्दी अनुवाद है, जिसमें वर्तमान को समझाने के लिए अतीत का सहारा लिया गया है। एक और सूफी की जबान से अतीत की घटनाएँ अनावृत्त होती जा रही हैं और दूसरी तरफ पाठकों के मन में मजहबी उन्माद की निरर्थकता घर कर जाती है। यह दो विरोधी संस्कृतियों के बीच शान्ति एवं सद्भाव का संदेश देता है।
मेलेप्पुल्लारा नामक हिन्दू परिवार और मुसलियारकम नामक मुसलमान परिवार के इर्द-गिर्द उपन्यास की घटनाएँ घटित होती हैं। दोनों परिवारों के अतीत की खोज से पता चलता है कि धर्म के नाम पर गर्व करने के लिए दोनों ही लायक नहीं हैं। इन दो परिवारों के लड़के-लड़की के मिलन का परिणाम सुखांत हो या न हो, अपनी कहानी के माध्यम से कथावाचक सूफी यही सीख देता है कि मजहब के नाम पर समाज का बँटवारा नहीं होना चाहिए। जात-पाँत के नाम पर खून-खराबा करने वाले लोग ईश्वर के दण्ड-विधान का शिकार बन जाते हैं। इतिहास की अन्तर्धाराओं को समझने की अगर हम जरा भी कोशिश करें तो आपसी बैर-विद्वेष की निरर्थकता हमारे सामने उजागर हो सकती है और साम्प्रदायिकता की खाई को पाटा जा सकता है।
उपन्यास के लेखक के.पी.रामनुण्णि (जन्म-1995,पोन्नानी, केरल) प्रतिष्ठित मलयाळम कथाकार हैं। सुफी परंज कथा (उपन्यास) के अलावा आपके आधा दर्जन कहानी-संग्रह प्रकाशित हैं। केरल साहित्य परिषद के समस्त पुरस्कारों सहित आपको केरल सहित्य अकादमी अवार्ड, इडश्शेरी अवार्ड, वि.पी. शिवकुमार स्मारक केलि अवार्ड, पद्रराजन पुरस्कार, कथा अवार्ड आदि अनेक पुरस्कार-सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। संप्रति आप तुंजन स्मारक ट्रस्ट में प्रशासक हैं और कोषिक्कोड में रहकर स्वतंत्र लेखन कार्य में रत हैं।
प्रस्तुत उपन्यास की अनुवादिका पी.के. राधमणि (जन्म-1982, त्रिश्शूर, केरल) ने हिन्दी भाषा एवं साहित्य में एम. ए., पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की हैं। हिन्दी और मलयाळम में आपकी एक-एक पुस्तक प्रकाशित है। संप्रति आप सलाबार क्रिश्चियन कॉलेज, कालिकट (केरल) में हिन्दी विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं।
मेलेप्पुल्लारा नामक हिन्दू परिवार और मुसलियारकम नामक मुसलमान परिवार के इर्द-गिर्द उपन्यास की घटनाएँ घटित होती हैं। दोनों परिवारों के अतीत की खोज से पता चलता है कि धर्म के नाम पर गर्व करने के लिए दोनों ही लायक नहीं हैं। इन दो परिवारों के लड़के-लड़की के मिलन का परिणाम सुखांत हो या न हो, अपनी कहानी के माध्यम से कथावाचक सूफी यही सीख देता है कि मजहब के नाम पर समाज का बँटवारा नहीं होना चाहिए। जात-पाँत के नाम पर खून-खराबा करने वाले लोग ईश्वर के दण्ड-विधान का शिकार बन जाते हैं। इतिहास की अन्तर्धाराओं को समझने की अगर हम जरा भी कोशिश करें तो आपसी बैर-विद्वेष की निरर्थकता हमारे सामने उजागर हो सकती है और साम्प्रदायिकता की खाई को पाटा जा सकता है।
उपन्यास के लेखक के.पी.रामनुण्णि (जन्म-1995,पोन्नानी, केरल) प्रतिष्ठित मलयाळम कथाकार हैं। सुफी परंज कथा (उपन्यास) के अलावा आपके आधा दर्जन कहानी-संग्रह प्रकाशित हैं। केरल साहित्य परिषद के समस्त पुरस्कारों सहित आपको केरल सहित्य अकादमी अवार्ड, इडश्शेरी अवार्ड, वि.पी. शिवकुमार स्मारक केलि अवार्ड, पद्रराजन पुरस्कार, कथा अवार्ड आदि अनेक पुरस्कार-सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। संप्रति आप तुंजन स्मारक ट्रस्ट में प्रशासक हैं और कोषिक्कोड में रहकर स्वतंत्र लेखन कार्य में रत हैं।
प्रस्तुत उपन्यास की अनुवादिका पी.के. राधमणि (जन्म-1982, त्रिश्शूर, केरल) ने हिन्दी भाषा एवं साहित्य में एम. ए., पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की हैं। हिन्दी और मलयाळम में आपकी एक-एक पुस्तक प्रकाशित है। संप्रति आप सलाबार क्रिश्चियन कॉलेज, कालिकट (केरल) में हिन्दी विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं।
अनुवादकीय
सांप्रदायिक विद्वेष तथा अलगाववादी तत्त्वों से प्रदूषित मध्यकालीन भारतीय परिवेश में आपसी भाई-चारे का संदेश फैलाने वाले सूफ़ी लोग भारतीय इतिहास के अभिन्न अंग हैं। सूफ़ी की ज़बान से सुनी कहानी के रूप में प्रस्तुत इस उपन्यास में भी दो विरोधी संस्कृतियों के बीच शांति एवं सद्भावना का संदेश मुखरित होता है।
मौजूदा विसंगितियों से जूझने के लिए साहित्यकार कभी-कभी मिथकों और पौराणिक पात्रों का सहारा लेते नज़र आते हैं। प्रस्तुत उपन्यास में भी वर्तमान को समझाने के लिए इतिहास का सहारा लिया गया है। एक और सूफ़ी की ज़बान से अतीत की घटनाएँ अनावृत होती जाती हैं और दूसरी तरफ़ पाठकों के मन में मज़हबी उन्माद की निरर्थकता घर कर जाती है।
हर युग में सृजन और संहार की शक्तियों का संघर्ष होता है। सत-असत की कशमकश हमेशा होती रहती है और संस्कृति एवं सभ्यता संकट में पड़ जाती है। युगीन साहित्य अपने समय की मूल्यहीनता को परखता है। मानव अस्तित्व और अस्मिता को ख़तरे में डालनेवाली दुविधाओं और समस्याओं की खोज करना साहित्यकारों का दायित्व है। मानव की मिथ्या आस्थाएँ उसे दानव मानते देखकर साहित्यकार की आत्मा को ठेस लग जाती है। उसे लगता है कि जैसा होना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं है। सब ओर विसंगतियाँ विराज रही हैं। मानव की बनावट इससे बेहतर होनी चाहिए। प्रस्तुत उपन्यास ऐसी ही एक मानसिकता की उपज है।
भारतीय समाज में इस्लाम के आगमन से दो संस्कृतियों का टकराव अवश्य हुआ था, मगर मात्र अलगाव की नहीं, बल्कि सामंजस्य की प्रवृत्तियाँ भी जाहिर हो रही थीं। सूफ़ियों ने समन्वय की यही भूमिका निभाई थी। सूफ़ी की कहानी भी यही भाषा बोलती है। आज सांप्रदायिकता, विघटन और विभाजन की ताक़त बनकर देश की भावात्मक एकता के लिए चुनौती बन चुकी है। मानव को धर्म और जातियों में बाँटनेवाली सांप्रदायिकता एक ख़तरनाक समस्या के रूप में समाज को निगलने के लिए मुँह बाए खड़ी है। इस नाम पर ख़ूनी संघर्ष भी कम नहीं हुआ करते। ऐसी हालत में इंसानियत को उजागर करना ज़रूरी हो गया है। एकता की ज़रूरत ज़ोरों से महसूस की जा रही है, मगर मरने-मारने पर उतारू होनेवाला धार्मिक उन्माद एकता के रास्ते का काँटा बना हुआ है। संवेदनशील साहित्यकार वर्तमान विसंगतियों से विचलित हुए बिना नहीं रह सकता। प्रस्तुत उपन्यास सूफ़ी दिलों को जोड़ने की कोशिश करके यही फ़र्ज़ अदा करता है। लेखक के साथ अगर हम भी यह मान ले कि तोड़कर अलग करते वक़्त रिश्तों की जो गर्मी भाप बनकर निकल जाती है, उसे वापस लाना मुश्किल है, तो तोड़ने के बदले हम जोड़ने की कोशिश करते हैं।
मेरेप्पुल्लारा नामक हिन्दू परिवार और मुसलियारकम नामक मुसलमान परिवार के इर्द-गिर्द उपन्यास की घटनाएँ घटित होती हैं। दोनों परिवारों के अतीत की खोज करने पर पता चलता है कि धर्म के नाम पर गर्व करने के लिए दोनों लायक़ नहीं हैं। इन दो परिवारों के लड़के-लड़की के मिलन का परिणाम सुखांत हो या न हो, अपनी कहानी के माध्यम से कथावाचक सूफ़ी यही सीख देता है कि मज़हब के नाम पर समाज का बँटवारा नहीं होना चाहिए। जात-पाँत के नाम पर ख़ून-ख़राबा करनेवाले लोग ईश्वर के दंड-विधान के शिकार बन जाते हैं। सबकी सब देवियाँ और बीबियाँ हिन्दू-मुसलमान के भेद-भाव के बिना सबकी अपनी हैं। ख़ून के रिश्तों से भी ज़्यादा मन के रिश्ते को महत्व देकर मामुट्टि की आत्मा के साथ एक होने के लिए अपना घर छोड़नेवाली कार्ति भी हमें यही सीख देती है कि इतिहास की अन्तर्धाराओं को समझने की अगर हम थोड़ी भी कोशिश करते तो आपसी वैर विद्वेष की निरर्थकता हमारी समझ में आ जाती और साम्प्रदायिकता यों संहारक रूप न धारण करती।
कार्ति के माध्यम से उपन्यासकार यह भी साबित करना चाहते हैं कि औरत सिर्फ़ भोग की वस्तु नहीं, उसके और भी कई आयाम हैं। जब कामरूपिणी एक कन्या का मातृरूप में परिवर्तन हो जाता है, तब वह भोग की नहीं, बल्कि पूजा की वस्तु बन जाती है। मातृत्व किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं मानता। वह सब पर कृपा करती है और सबकी देखभाल करती है। प्रस्तुत उपन्यास की बीवी जाति भेद के बिना अपने पास पहुँचने वाले सब लोगों की मुरादें पूरी कर देती है। जाति के आधार पर कोई भी माता अपनी संतानों का विभाजन नहीं कर सकती है। अपनी कोख से संतानों को जन्म न देकर भी उपन्यास की नायिका कार्ति विश्वमाता के उन्नत आसन पर विराजमान होकर अमर बन जाती है।
कार्ति अति संयमित और अतिशय ताक़तवर औरत है। स्त्री का धर्म देखनेवालों को कामातुर करना और उसके अंगों को ऊष्मा से भर देना मात्र नहीं है। कितना अघट घट गया कि मामुट्टि को कीर्ति से वितृष्णा हो गई। आँखों से पाषाणी भाव और होंठों पर बर्फ़ सी जमी कठोरता के साथ मामुट्टि कार्ति की अवहेलना करने लगता है, लेकिन कार्ति चूँ तक नहीं करती। अहं को चोट लगती है तो मामुट्टि बरदाश्त नहीं कर पाता। कार्ति के समर्पण और त्याग को वह भूल जाता है और उसकी उपेक्षा करता है। लेकिन मामुट्टि का बदला हुआ चेहरा देखकर भी कार्ति नाज-नखरे नहीं करती या क्रोध की आग में नहीं जलती। उपन्यास में कभी भी कार्ति के मानसिक धरातल की ऊँचाई तक मामुट्टि अपने को नहीं उठा पाता।
मातृत्व स्त्री की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। एक संरक्षक माता के रूप में कार्ति के परिणाम में उपन्यास की दार्शनिकता सार्थक हो जाती है। ‘सर्वभूतेषु’ मातृरूपेण संस्थिता’ देवी अपनी संतानों में भेदभाव नहीं रख सकती।
थोड़े शब्दों में अनुवाद की पूर्वपीठिका प्रस्तुत करना यहाँ अनिवार्य है। पहली बार इस उपन्यास को पढ़ा, तो उसके अनुवाद करने का कोई इरादा मन में नहीं था। लेकिन कार्ति का नजा़कत और ताक़त कभी ख़ुशबू बन महकने और कभी सुई की चुभन बन गहराई में दर्द देने लगी तो इस उपन्यास के साथ गहरा रिश्ता क़ायम करने के लिए मन तरसने लगा। खोजने पर पता चला कि प्रस्तुत उपन्यास का अंग्रेज़ी अनुवादक श्री. एन.गोपालकृष्णन अपने कॉलेज के अंग्रेज़ी विभाग की अध्यक्षता डॉ. लिसी मांजुरान के पड़ोसी है। इस बीच में लेखक श्री रामनुण्णि से भी अनुवाद के सिलसिले में बात कर चुकी थी। श्री गोपालकृष्णन के घर में हम मिले। उपन्यास की भाषा और शैली कुछ अनूठी होने के कारण अनुवाद की सफलता के संबंध में मन संदेह अवश्य था, लेकिन लेखक रामनुण्णि ने यह कहकर कि लुक रोजर नामक एक फ्रांसीसी फ़िलोलोजिस्ट इस उपन्यास का फ्रेंच अनुवाद कर रहे हैं, मुझे धीरज बँधाया। एक विदेशी भाषा में अनुवाद संभव है, तो हिंदी अनुवाद की सफलता को लेकर परेशान होने की बात ही नहीं।
ख़ैर अनुवाद पूरा हुआ और मुझे लगा कि हिन्दी के ज्ञाता किसी सहृदय विद्वान के द्वारा इसकी छानबीन करवाना अनिवार्य है, ताकि अपनी मातृभाषा के प्रभाव से घुसपैठ करनेवाली अस्वाभाविक लेखन शैलियों को पहचानकर अशुद्धियों को सुधार सकूँ। श्री रामनुण्णि ने अपनी इस समस्या का हल निकाल दिया। उन्होंने मलयाळम् और अंग्रेज़ी के विद्वान लेखक तथा पुस्तक के अंग्रेज़ी अनुवादक श्री एन. गोपालकृष्णन का नाम सुझाया। वे नौकरी के सिलसिले में कई सालों तक हिन्दी प्रदेशों में रह चुके थे। मुझे उनके साथ अपनी पहली मुलाकात याद आई। उस वक़्त मूँछों पर ताव देकर बैठे उस अग्रज बंधु की आंखों में दोस्ती की किरणों की चमक मैं नहीं देख पाई थी। लेकिन श्री रामनुण्णि के सुझाव पर जब मैं उनके घर दुबारा पहुँच गई तो ज़िन्दगी में पहली बार मैंने जाना कि लोगों को समझने में मैं कितनी अनाड़ी हूँ। लगातार तीन दिनों तक वे मेरे साथ बैठे। बिना ऊबे, बिना जम्हाई लिए एक-एक वाक्य को बड़े ध्यान से सुना और आवश्यक संशोधन कर दिया। उनके प्रति आभार व्यक्त करना मेरे बस की बात नहीं। मैं उन चरणों के आगे नतमस्तक हो जाती हूँ।
अनुवाद के दिग्गज पंडितों की केरल में कोई कमी नहीं। फिर भी जाने किस दैवी प्रेरणा से लेखक श्री रामनुण्णि ने मुझ अजनबी पर भरोसा करके अनुवाद का काम मुझको सौंप दिया, मैं तहे दिल से उनके प्रति आभारी हूँ।
केन्द्रीय साहित्य अकादमी ने प्रकाशन का दायित्व ले लिया, मैं अनुगृहीत हुई।
मौजूदा विसंगितियों से जूझने के लिए साहित्यकार कभी-कभी मिथकों और पौराणिक पात्रों का सहारा लेते नज़र आते हैं। प्रस्तुत उपन्यास में भी वर्तमान को समझाने के लिए इतिहास का सहारा लिया गया है। एक और सूफ़ी की ज़बान से अतीत की घटनाएँ अनावृत होती जाती हैं और दूसरी तरफ़ पाठकों के मन में मज़हबी उन्माद की निरर्थकता घर कर जाती है।
हर युग में सृजन और संहार की शक्तियों का संघर्ष होता है। सत-असत की कशमकश हमेशा होती रहती है और संस्कृति एवं सभ्यता संकट में पड़ जाती है। युगीन साहित्य अपने समय की मूल्यहीनता को परखता है। मानव अस्तित्व और अस्मिता को ख़तरे में डालनेवाली दुविधाओं और समस्याओं की खोज करना साहित्यकारों का दायित्व है। मानव की मिथ्या आस्थाएँ उसे दानव मानते देखकर साहित्यकार की आत्मा को ठेस लग जाती है। उसे लगता है कि जैसा होना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं है। सब ओर विसंगतियाँ विराज रही हैं। मानव की बनावट इससे बेहतर होनी चाहिए। प्रस्तुत उपन्यास ऐसी ही एक मानसिकता की उपज है।
भारतीय समाज में इस्लाम के आगमन से दो संस्कृतियों का टकराव अवश्य हुआ था, मगर मात्र अलगाव की नहीं, बल्कि सामंजस्य की प्रवृत्तियाँ भी जाहिर हो रही थीं। सूफ़ियों ने समन्वय की यही भूमिका निभाई थी। सूफ़ी की कहानी भी यही भाषा बोलती है। आज सांप्रदायिकता, विघटन और विभाजन की ताक़त बनकर देश की भावात्मक एकता के लिए चुनौती बन चुकी है। मानव को धर्म और जातियों में बाँटनेवाली सांप्रदायिकता एक ख़तरनाक समस्या के रूप में समाज को निगलने के लिए मुँह बाए खड़ी है। इस नाम पर ख़ूनी संघर्ष भी कम नहीं हुआ करते। ऐसी हालत में इंसानियत को उजागर करना ज़रूरी हो गया है। एकता की ज़रूरत ज़ोरों से महसूस की जा रही है, मगर मरने-मारने पर उतारू होनेवाला धार्मिक उन्माद एकता के रास्ते का काँटा बना हुआ है। संवेदनशील साहित्यकार वर्तमान विसंगतियों से विचलित हुए बिना नहीं रह सकता। प्रस्तुत उपन्यास सूफ़ी दिलों को जोड़ने की कोशिश करके यही फ़र्ज़ अदा करता है। लेखक के साथ अगर हम भी यह मान ले कि तोड़कर अलग करते वक़्त रिश्तों की जो गर्मी भाप बनकर निकल जाती है, उसे वापस लाना मुश्किल है, तो तोड़ने के बदले हम जोड़ने की कोशिश करते हैं।
मेरेप्पुल्लारा नामक हिन्दू परिवार और मुसलियारकम नामक मुसलमान परिवार के इर्द-गिर्द उपन्यास की घटनाएँ घटित होती हैं। दोनों परिवारों के अतीत की खोज करने पर पता चलता है कि धर्म के नाम पर गर्व करने के लिए दोनों लायक़ नहीं हैं। इन दो परिवारों के लड़के-लड़की के मिलन का परिणाम सुखांत हो या न हो, अपनी कहानी के माध्यम से कथावाचक सूफ़ी यही सीख देता है कि मज़हब के नाम पर समाज का बँटवारा नहीं होना चाहिए। जात-पाँत के नाम पर ख़ून-ख़राबा करनेवाले लोग ईश्वर के दंड-विधान के शिकार बन जाते हैं। सबकी सब देवियाँ और बीबियाँ हिन्दू-मुसलमान के भेद-भाव के बिना सबकी अपनी हैं। ख़ून के रिश्तों से भी ज़्यादा मन के रिश्ते को महत्व देकर मामुट्टि की आत्मा के साथ एक होने के लिए अपना घर छोड़नेवाली कार्ति भी हमें यही सीख देती है कि इतिहास की अन्तर्धाराओं को समझने की अगर हम थोड़ी भी कोशिश करते तो आपसी वैर विद्वेष की निरर्थकता हमारी समझ में आ जाती और साम्प्रदायिकता यों संहारक रूप न धारण करती।
कार्ति के माध्यम से उपन्यासकार यह भी साबित करना चाहते हैं कि औरत सिर्फ़ भोग की वस्तु नहीं, उसके और भी कई आयाम हैं। जब कामरूपिणी एक कन्या का मातृरूप में परिवर्तन हो जाता है, तब वह भोग की नहीं, बल्कि पूजा की वस्तु बन जाती है। मातृत्व किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं मानता। वह सब पर कृपा करती है और सबकी देखभाल करती है। प्रस्तुत उपन्यास की बीवी जाति भेद के बिना अपने पास पहुँचने वाले सब लोगों की मुरादें पूरी कर देती है। जाति के आधार पर कोई भी माता अपनी संतानों का विभाजन नहीं कर सकती है। अपनी कोख से संतानों को जन्म न देकर भी उपन्यास की नायिका कार्ति विश्वमाता के उन्नत आसन पर विराजमान होकर अमर बन जाती है।
कार्ति अति संयमित और अतिशय ताक़तवर औरत है। स्त्री का धर्म देखनेवालों को कामातुर करना और उसके अंगों को ऊष्मा से भर देना मात्र नहीं है। कितना अघट घट गया कि मामुट्टि को कीर्ति से वितृष्णा हो गई। आँखों से पाषाणी भाव और होंठों पर बर्फ़ सी जमी कठोरता के साथ मामुट्टि कार्ति की अवहेलना करने लगता है, लेकिन कार्ति चूँ तक नहीं करती। अहं को चोट लगती है तो मामुट्टि बरदाश्त नहीं कर पाता। कार्ति के समर्पण और त्याग को वह भूल जाता है और उसकी उपेक्षा करता है। लेकिन मामुट्टि का बदला हुआ चेहरा देखकर भी कार्ति नाज-नखरे नहीं करती या क्रोध की आग में नहीं जलती। उपन्यास में कभी भी कार्ति के मानसिक धरातल की ऊँचाई तक मामुट्टि अपने को नहीं उठा पाता।
मातृत्व स्त्री की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। एक संरक्षक माता के रूप में कार्ति के परिणाम में उपन्यास की दार्शनिकता सार्थक हो जाती है। ‘सर्वभूतेषु’ मातृरूपेण संस्थिता’ देवी अपनी संतानों में भेदभाव नहीं रख सकती।
थोड़े शब्दों में अनुवाद की पूर्वपीठिका प्रस्तुत करना यहाँ अनिवार्य है। पहली बार इस उपन्यास को पढ़ा, तो उसके अनुवाद करने का कोई इरादा मन में नहीं था। लेकिन कार्ति का नजा़कत और ताक़त कभी ख़ुशबू बन महकने और कभी सुई की चुभन बन गहराई में दर्द देने लगी तो इस उपन्यास के साथ गहरा रिश्ता क़ायम करने के लिए मन तरसने लगा। खोजने पर पता चला कि प्रस्तुत उपन्यास का अंग्रेज़ी अनुवादक श्री. एन.गोपालकृष्णन अपने कॉलेज के अंग्रेज़ी विभाग की अध्यक्षता डॉ. लिसी मांजुरान के पड़ोसी है। इस बीच में लेखक श्री रामनुण्णि से भी अनुवाद के सिलसिले में बात कर चुकी थी। श्री गोपालकृष्णन के घर में हम मिले। उपन्यास की भाषा और शैली कुछ अनूठी होने के कारण अनुवाद की सफलता के संबंध में मन संदेह अवश्य था, लेकिन लेखक रामनुण्णि ने यह कहकर कि लुक रोजर नामक एक फ्रांसीसी फ़िलोलोजिस्ट इस उपन्यास का फ्रेंच अनुवाद कर रहे हैं, मुझे धीरज बँधाया। एक विदेशी भाषा में अनुवाद संभव है, तो हिंदी अनुवाद की सफलता को लेकर परेशान होने की बात ही नहीं।
ख़ैर अनुवाद पूरा हुआ और मुझे लगा कि हिन्दी के ज्ञाता किसी सहृदय विद्वान के द्वारा इसकी छानबीन करवाना अनिवार्य है, ताकि अपनी मातृभाषा के प्रभाव से घुसपैठ करनेवाली अस्वाभाविक लेखन शैलियों को पहचानकर अशुद्धियों को सुधार सकूँ। श्री रामनुण्णि ने अपनी इस समस्या का हल निकाल दिया। उन्होंने मलयाळम् और अंग्रेज़ी के विद्वान लेखक तथा पुस्तक के अंग्रेज़ी अनुवादक श्री एन. गोपालकृष्णन का नाम सुझाया। वे नौकरी के सिलसिले में कई सालों तक हिन्दी प्रदेशों में रह चुके थे। मुझे उनके साथ अपनी पहली मुलाकात याद आई। उस वक़्त मूँछों पर ताव देकर बैठे उस अग्रज बंधु की आंखों में दोस्ती की किरणों की चमक मैं नहीं देख पाई थी। लेकिन श्री रामनुण्णि के सुझाव पर जब मैं उनके घर दुबारा पहुँच गई तो ज़िन्दगी में पहली बार मैंने जाना कि लोगों को समझने में मैं कितनी अनाड़ी हूँ। लगातार तीन दिनों तक वे मेरे साथ बैठे। बिना ऊबे, बिना जम्हाई लिए एक-एक वाक्य को बड़े ध्यान से सुना और आवश्यक संशोधन कर दिया। उनके प्रति आभार व्यक्त करना मेरे बस की बात नहीं। मैं उन चरणों के आगे नतमस्तक हो जाती हूँ।
अनुवाद के दिग्गज पंडितों की केरल में कोई कमी नहीं। फिर भी जाने किस दैवी प्रेरणा से लेखक श्री रामनुण्णि ने मुझ अजनबी पर भरोसा करके अनुवाद का काम मुझको सौंप दिया, मैं तहे दिल से उनके प्रति आभारी हूँ।
केन्द्रीय साहित्य अकादमी ने प्रकाशन का दायित्व ले लिया, मैं अनुगृहीत हुई।
एक
सागर किनारे बीबी की क़ब्र उठी तो हक़ीक़त और युक्ति के कोष्ठों में उकता गए हम बस्तीवाले बड़े खुश हो गए। अंधविश्वास है तो भी क्या बुरा ?
अर्से से मात्र यथार्थ की कठोरता में विश्वास करना सीखकर हमने क्या पाया ? काल्पनिकता के चरागाहों को दफ़नाकर धरती झुलस गई। भ्रम की सिलवटों में ही सही, स्त्रवित हमारे मन बंजर हो गए। जाति भेद के बिना सब पर कृपा करनेवाले मूसान औलिया और कंडेन चिरक्कल देवी की दिव्य शक्तियाँ मिटर दी गईं। और बदले में किसी नई शक्ति का आसरा हमें दिया गया ? वह भी नहीं। इसलिए आज जो बीबी हमें राहत दिलाने आई है, उसे हम सुना-सुनाई सभी अतिरंजित कथाओं के साथ सागर तट पर ही नहीं, बल्कि अपने मन में भी प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं।
नास्तिकों ने मज़ार के ख़िलाफ़ नोटिस निकाली थी। गुस्से में आकर मैंने नौटिस फेंक दी। वाह रे नास्तिक, एक नई संकल्पना के कोंपल को इस धरती पर उगने नहीं दोगे ?
सायंकालीन सुस्त समीर में बीबी की दरगाह की ओर मैं बह चला। तट की तरफ़ जानेवाली सड़क पर घुसते ही सागर की कराहों ने मुझमें अनंत व्यथाओं का तूफ़ान उठाया। मैंने ख़ुद को समझाने की कोशिश की कि बेवजह मुसीबतों की गिरफ़्त से हमें बचाने के लिए ही बीबी सागर तट पर पहुँच गई हैं और इस ख़याल से मुझे रोना आया।
सांप्रदायिक दंगा और दो गुटों के बीच शत्रुता के फलस्वरूप सारी मुसीबतों की शुरूआत हो गई थी। अब भी समझ में नहीं आता कि सालों तक एक-दूसरे के त्योहारों में शरीक होकर, बारी-बारी से ओणम और ईद की दावत खाते आ रहे हमलोगों को अचानक क्या हो गया था।
अशुभ के आगमन की सूचना ज्यों इलाक़े में हैजा फैल गया। आसमान में उठे बादलों के खंभों ने बदला लेने के अंदाज़ में नीचे ढहकर हमारे कगारों को कुतर लिया। प्यार के बदले कलेजा निकालकर देनेवाले, बेईमान पर गाली-गलौज और मारपीट पर उतर आनेवाले मन के भोले मछुआरे सागर में मरे।
नागदेवता की चौक के आस पास झुरमुटों के बीच पल रहे मोटे-तगड़े सियार अचानक पागल हो गए। पागल सियारों के झुण्ड ने पालतू कुत्तों को काटा। कई हिन्दू लड़के पागल कुत्तों के काटने से अस्पताल में भर्ती हो गए। वे सब एक-एक करके पागल बन, पानी के लिए तरस-तरसकर मरे।
किसी सातत्य की कड़ियाँ ज्यों जगह-जगह पर मुसीबतों ने घेरा डाला।
सांप्रदायिक दुश्मनी भूलकर पहलेवाला सद्भाव क़याम करने के इरादे से हिन्दू और मुसलमान बिरियानी और खीर खाने के लिए एक-दूसरे के घर गए। लेकिन दोनों के दिलों में उमस तब भी बाक़ी थी। तोड़कर अलग करते वक़्त रिश्तों की जो गर्मी भाप बनकर बाहर निकलती है, उसे वापस पाना मुश्किल है।
सब कुछ देखकर धरती माँ मन मसोसकर रह गई थी और आज वह बीबी बनकर अवतरित हुई है। हिन्दू हो या मुसलमान, नारियल तेल और अगरबत्ती के भेंट चढ़ाकर मनौती माँगी तो भेदभाव के बिना सबकी मुरादें पूरी हो जातीं हैं।
दुःखी देशवासियों की भीड़ के साथ मैं बीबी नगरवाले रेतीले पथ पर मुड़ गया।
‘‘बीबी...ओ मेरी बीबी।’’
निश्वासों में जप मालाएँ अटक गईं। मेरा गला रुँध गया। शाम ढल चुकी थी। काले पड़ते सागर की बाँहें बीबी की आधीनता को स्वीकार करने की मुद्रा में अंजलिबद्ध होकर ऊपर को उठ रही थीं। किसी गहन तूफ़ान के झोंके की तरह आसमान से ठंड नीचे उतर रही थी।
इधर-उधर नारियल के पत्तों से बनी दुकानों में सूरज के रूप में पेट्रोमैक्स चमक रहे थे। बचपन में पेट्रोमैक्स का प्रकाश मुझमें एक अजीब उत्साह भर देता था। हर कहीं समारोह का साथी बननेवाली यह बत्ती उमंगों का प्रतीक है।
‘‘बीबी के लिए नारियल ले तेल ले जाओ।’
‘‘बीबी के लिए अगरबत्ती ले आओ।’’
‘‘इधर, इस तरफ़ आओ।’’ दुकानों में व्यापारी प्यार भरी आवाज़ में बीबी के भक्तों को पुकार रहे थे।
गोद में और हाथों में लटकते टकले बच्चों के साथ एक मुसलमान औरत दुकान में घूसी तो मैं भी उसके पीछे-पीछे चलने लगा। अचानक मिल जाने वाले सहयात्रियों के साथ दोस्ती निभाना और उनके साथ हो लेना मेरी कमज़ोरी है। मुसलमान बहन ने एक छोटे कनस्तर में सौ मिली लीटर नारियल तेल और अगरबत्ती का एक चपटा पैकेट खरीदा तो मैंने भी उसी अनुपात में चीज़ें ख़रीदीं। हर कार्य में उसका अनुकरण कर पीछे मुझ अजनबी की ओर उसने वात्सल्य भरी निगाहों से देखा।
रेत को कुचलकर आगे बढ़ रहे हमारे पैर निद्राचारियों के से हो गए। दरगाह के पास पहुँचने पर चारों ओर उछलती प्रकाश धारा में मैंने उसके चेहरे की ओर ग़ौर किया। वहाँ पाँच-छह बच्चों के सँभालने की परेशानी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि बीबी के दर्शन का भावावेग मात्र प्रकट था। दबी गुर्राहट ज्यों अंदर से निकलती मंत्र-ध्वनियों के ऊपर वह पुकार उठी, ‘‘चल रही...जल्दी चल...।’’
अपने नन्हें पैरों को घसीटकर रेत के ऊपर से बड़ी कठिनाई से चली आ रही उसकी बेटियाँ आनन-फ़ानन आगे की ओर दौड़ पड़ीं। औरतों के लिए अलग जगह बनाई गई थी। वे सब एक जुट होकर उस तरफ़ निकलीं तो मैं भी अपने रास्ते चला। दरगाह के अन्दर तेल की गंध और अगरबत्ती की धूम के कारण बने तरल वातावरण में, मैं कोख के अंदर हाथ पैर पटकता बच्चा बन गया।
क़ब्र के सामनेवाली क्यू में आगे बढ़ते समय सिर पर साफ़ा बाँधे, दाढ़ीवाले लोग सफ़ेद कपड़ों में क़ुरआन की आयतों का पाठ करते या मंत्रों का जप करते दिखाई दिए। उनकी उँगलियों में जप मालाएँ फिर रही थी। क़ब्र के सामने पहुँचते ही एक मौलवी ने वात्सल्य भाव से मेरे हाथ से तेल का डिब्बा ले लिया। उसमें से थोड़ा तेल दीये में डालने के बाद उसने बाक़ी मुझे लौटा दिया।
क़ब्र को छूने की व्यग्रता में शायद मैंने क़तार में कुछ गड़बड़ी की होगी। मेरा उतावलापन देखकर कुछ दूर अदब से खड़े एक दाढ़ी वाले ने आगे आकर मेरी उँगली पकड़कर क़ब्र को छुआ दिया और क़तार से आज़ाद करके एक-दूसरे रास्ते से मुझे बाहर ले आया।
बाहर ही अंदर का वातावरण, नमी का उबटन ज्यों मेरे मन में शेष रहा। सफ़ेद दाढ़ी-मूँछवाले उस बूढ़े बाबा के हाथों की गर्मी में राहत पा रहा था। मैंने याद करने की कोशिश की—यों एक चेहरा मैंने पहले कहाँ देखा ? तस्वीरों में, शिल्पों में या पुरानी खोपड़ियों में जाने कहाँ मैंने इस चेहरे को भुला दिया था। बाबा की उँगलियों की नगदार अँगूठियों की चमक में मेरी आँखें चौंधिया गईं।
क्या ये कोई सूफ़ी या सिद्ध महात्मा हैं। सुना है, ऐसे लोग सैकड़ों साल ज़िन्दा रहते हैं और सागरों को आसानी से पार कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए असलियत के चक्कर से बाहर निकलने का मौक़ा मिला तो मैंने ख़ुशी-ख़ुशी उनकी आधीनता स्वीकार की। चाहे ये मुझ पर अपना जादू चला लें या कोई ज़हर ही मुझे पिला दें, मगर उस वक़्त मुझे ऐसे ख़यालों से डर नहीं लगा।
एक-दूसरे से थोड़ा हटकर सागर की ओर देखकर हम तट पर बैठ गए। मणि जड़ित अँगूठियोंवाली उँगलियों से, उन हाथों से, छाती से और तिकोने जबड़े की घनी दाढ़ी से गुज़रकर मेरी नज़र उनकी झील जैसी आँखों में जा रुकी। तब पहली बार उन्होंने मुँह खोला।
‘‘बेटा, तुम इसी इलाक़े के हो ना ?’’
‘‘जी हाँ।’’
‘‘हिन्दू हो ?’’
‘‘हाँ।’’
‘‘बीबियों और देवियों की कहानियों की खोज में निकले हो ?’’
‘‘हाँ, हाँ वही।’’
‘‘हमारे देश में सैकड़ों ऐसी कहानियाँ भुला दी गई हैं। सुनना चाहोगे ?’’
‘‘हाँ-हाँ, बिलकुल।’’
जिस आदमी की उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, उसके अद्भुत ज्ञान के संबंध में मुझे कोई संदेह नहीं हुआ। देश के विभिन्न इलाक़ों की दंत कथाओं और जनश्रुतियों की खोज में निकला मैं मालिक के पास बैठे आज्ञाकारी कुत्ते की तरह, आदर के साथ, उस बूढ़े बाबा से चिपककर बैठ गया।
‘‘बेटा, जानते हो इस बीबी की कौन-सी बारी है ?’’
‘‘नहीं।’’
‘‘यह हमारे देश के तीसरी बीबी है। और भी न जाने कितने देवी-देवता इस देश में हुए हैं। इनके अलावा कई औलिया भी हैं। सबकी अपनी-अपनी दंत कथाएँ हैं। ये सब किसकी संपदा हैं ?’’
‘‘क्यों ? हम सबकी।’’
‘‘तुमने सही कहा। सारे-के-सारे देवी-देवता, औलिया और बीबियाँ सबके सब हमारे अपने हैं। जिस तरह ये बीबियाँ, बेटा तुम्हारी हैं यद्यपि हिन्दू हो, उसी तरह ये देवी-देवता मेरे भी हैं, यद्यपि मैं मुसलमान हूँ।’’
‘‘पहली बीबी तुम्हारे समुदाय की थी। जी हाँ, वह एक हिन्दू नायर खानदान की औरत थी। मेलेप्पुल्लारा ख़ानदान के बारे में सुना है ? आज उस खानदान में कोई भी ज़िन्दा नहीं। उसका विनाश हो गया। अच्छा, वह कहानी मैं तुम्हें सुना देता हूँ।’’
किसी विस्तृत मंत्र-ध्वनी की तरह उस ख़ानदान का नाम मेरे अंदर गूँज उठा। विश्व कथाकार ऋषि के साये में जैसे, मैं उस कहानी में विलीन हुआ। उनके शब्द तस्वीर बन प्रवाहित होने लगे। मेलेप्पुल्लारा हवेली की ओर जानेवाली लाल मिट्टी की चक्करदार सड़क दृश्यमान हो गई। बाबा की झील-सी आँखें और दाढ़ी के उलझे हुए सफ़ेद बाल सबकी गवाही देते प्रतीत हो रहे थे।
अर्से से मात्र यथार्थ की कठोरता में विश्वास करना सीखकर हमने क्या पाया ? काल्पनिकता के चरागाहों को दफ़नाकर धरती झुलस गई। भ्रम की सिलवटों में ही सही, स्त्रवित हमारे मन बंजर हो गए। जाति भेद के बिना सब पर कृपा करनेवाले मूसान औलिया और कंडेन चिरक्कल देवी की दिव्य शक्तियाँ मिटर दी गईं। और बदले में किसी नई शक्ति का आसरा हमें दिया गया ? वह भी नहीं। इसलिए आज जो बीबी हमें राहत दिलाने आई है, उसे हम सुना-सुनाई सभी अतिरंजित कथाओं के साथ सागर तट पर ही नहीं, बल्कि अपने मन में भी प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं।
नास्तिकों ने मज़ार के ख़िलाफ़ नोटिस निकाली थी। गुस्से में आकर मैंने नौटिस फेंक दी। वाह रे नास्तिक, एक नई संकल्पना के कोंपल को इस धरती पर उगने नहीं दोगे ?
सायंकालीन सुस्त समीर में बीबी की दरगाह की ओर मैं बह चला। तट की तरफ़ जानेवाली सड़क पर घुसते ही सागर की कराहों ने मुझमें अनंत व्यथाओं का तूफ़ान उठाया। मैंने ख़ुद को समझाने की कोशिश की कि बेवजह मुसीबतों की गिरफ़्त से हमें बचाने के लिए ही बीबी सागर तट पर पहुँच गई हैं और इस ख़याल से मुझे रोना आया।
सांप्रदायिक दंगा और दो गुटों के बीच शत्रुता के फलस्वरूप सारी मुसीबतों की शुरूआत हो गई थी। अब भी समझ में नहीं आता कि सालों तक एक-दूसरे के त्योहारों में शरीक होकर, बारी-बारी से ओणम और ईद की दावत खाते आ रहे हमलोगों को अचानक क्या हो गया था।
अशुभ के आगमन की सूचना ज्यों इलाक़े में हैजा फैल गया। आसमान में उठे बादलों के खंभों ने बदला लेने के अंदाज़ में नीचे ढहकर हमारे कगारों को कुतर लिया। प्यार के बदले कलेजा निकालकर देनेवाले, बेईमान पर गाली-गलौज और मारपीट पर उतर आनेवाले मन के भोले मछुआरे सागर में मरे।
नागदेवता की चौक के आस पास झुरमुटों के बीच पल रहे मोटे-तगड़े सियार अचानक पागल हो गए। पागल सियारों के झुण्ड ने पालतू कुत्तों को काटा। कई हिन्दू लड़के पागल कुत्तों के काटने से अस्पताल में भर्ती हो गए। वे सब एक-एक करके पागल बन, पानी के लिए तरस-तरसकर मरे।
किसी सातत्य की कड़ियाँ ज्यों जगह-जगह पर मुसीबतों ने घेरा डाला।
सांप्रदायिक दुश्मनी भूलकर पहलेवाला सद्भाव क़याम करने के इरादे से हिन्दू और मुसलमान बिरियानी और खीर खाने के लिए एक-दूसरे के घर गए। लेकिन दोनों के दिलों में उमस तब भी बाक़ी थी। तोड़कर अलग करते वक़्त रिश्तों की जो गर्मी भाप बनकर बाहर निकलती है, उसे वापस पाना मुश्किल है।
सब कुछ देखकर धरती माँ मन मसोसकर रह गई थी और आज वह बीबी बनकर अवतरित हुई है। हिन्दू हो या मुसलमान, नारियल तेल और अगरबत्ती के भेंट चढ़ाकर मनौती माँगी तो भेदभाव के बिना सबकी मुरादें पूरी हो जातीं हैं।
दुःखी देशवासियों की भीड़ के साथ मैं बीबी नगरवाले रेतीले पथ पर मुड़ गया।
‘‘बीबी...ओ मेरी बीबी।’’
निश्वासों में जप मालाएँ अटक गईं। मेरा गला रुँध गया। शाम ढल चुकी थी। काले पड़ते सागर की बाँहें बीबी की आधीनता को स्वीकार करने की मुद्रा में अंजलिबद्ध होकर ऊपर को उठ रही थीं। किसी गहन तूफ़ान के झोंके की तरह आसमान से ठंड नीचे उतर रही थी।
इधर-उधर नारियल के पत्तों से बनी दुकानों में सूरज के रूप में पेट्रोमैक्स चमक रहे थे। बचपन में पेट्रोमैक्स का प्रकाश मुझमें एक अजीब उत्साह भर देता था। हर कहीं समारोह का साथी बननेवाली यह बत्ती उमंगों का प्रतीक है।
‘‘बीबी के लिए नारियल ले तेल ले जाओ।’
‘‘बीबी के लिए अगरबत्ती ले आओ।’’
‘‘इधर, इस तरफ़ आओ।’’ दुकानों में व्यापारी प्यार भरी आवाज़ में बीबी के भक्तों को पुकार रहे थे।
गोद में और हाथों में लटकते टकले बच्चों के साथ एक मुसलमान औरत दुकान में घूसी तो मैं भी उसके पीछे-पीछे चलने लगा। अचानक मिल जाने वाले सहयात्रियों के साथ दोस्ती निभाना और उनके साथ हो लेना मेरी कमज़ोरी है। मुसलमान बहन ने एक छोटे कनस्तर में सौ मिली लीटर नारियल तेल और अगरबत्ती का एक चपटा पैकेट खरीदा तो मैंने भी उसी अनुपात में चीज़ें ख़रीदीं। हर कार्य में उसका अनुकरण कर पीछे मुझ अजनबी की ओर उसने वात्सल्य भरी निगाहों से देखा।
रेत को कुचलकर आगे बढ़ रहे हमारे पैर निद्राचारियों के से हो गए। दरगाह के पास पहुँचने पर चारों ओर उछलती प्रकाश धारा में मैंने उसके चेहरे की ओर ग़ौर किया। वहाँ पाँच-छह बच्चों के सँभालने की परेशानी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि बीबी के दर्शन का भावावेग मात्र प्रकट था। दबी गुर्राहट ज्यों अंदर से निकलती मंत्र-ध्वनियों के ऊपर वह पुकार उठी, ‘‘चल रही...जल्दी चल...।’’
अपने नन्हें पैरों को घसीटकर रेत के ऊपर से बड़ी कठिनाई से चली आ रही उसकी बेटियाँ आनन-फ़ानन आगे की ओर दौड़ पड़ीं। औरतों के लिए अलग जगह बनाई गई थी। वे सब एक जुट होकर उस तरफ़ निकलीं तो मैं भी अपने रास्ते चला। दरगाह के अन्दर तेल की गंध और अगरबत्ती की धूम के कारण बने तरल वातावरण में, मैं कोख के अंदर हाथ पैर पटकता बच्चा बन गया।
क़ब्र के सामनेवाली क्यू में आगे बढ़ते समय सिर पर साफ़ा बाँधे, दाढ़ीवाले लोग सफ़ेद कपड़ों में क़ुरआन की आयतों का पाठ करते या मंत्रों का जप करते दिखाई दिए। उनकी उँगलियों में जप मालाएँ फिर रही थी। क़ब्र के सामने पहुँचते ही एक मौलवी ने वात्सल्य भाव से मेरे हाथ से तेल का डिब्बा ले लिया। उसमें से थोड़ा तेल दीये में डालने के बाद उसने बाक़ी मुझे लौटा दिया।
क़ब्र को छूने की व्यग्रता में शायद मैंने क़तार में कुछ गड़बड़ी की होगी। मेरा उतावलापन देखकर कुछ दूर अदब से खड़े एक दाढ़ी वाले ने आगे आकर मेरी उँगली पकड़कर क़ब्र को छुआ दिया और क़तार से आज़ाद करके एक-दूसरे रास्ते से मुझे बाहर ले आया।
बाहर ही अंदर का वातावरण, नमी का उबटन ज्यों मेरे मन में शेष रहा। सफ़ेद दाढ़ी-मूँछवाले उस बूढ़े बाबा के हाथों की गर्मी में राहत पा रहा था। मैंने याद करने की कोशिश की—यों एक चेहरा मैंने पहले कहाँ देखा ? तस्वीरों में, शिल्पों में या पुरानी खोपड़ियों में जाने कहाँ मैंने इस चेहरे को भुला दिया था। बाबा की उँगलियों की नगदार अँगूठियों की चमक में मेरी आँखें चौंधिया गईं।
क्या ये कोई सूफ़ी या सिद्ध महात्मा हैं। सुना है, ऐसे लोग सैकड़ों साल ज़िन्दा रहते हैं और सागरों को आसानी से पार कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए असलियत के चक्कर से बाहर निकलने का मौक़ा मिला तो मैंने ख़ुशी-ख़ुशी उनकी आधीनता स्वीकार की। चाहे ये मुझ पर अपना जादू चला लें या कोई ज़हर ही मुझे पिला दें, मगर उस वक़्त मुझे ऐसे ख़यालों से डर नहीं लगा।
एक-दूसरे से थोड़ा हटकर सागर की ओर देखकर हम तट पर बैठ गए। मणि जड़ित अँगूठियोंवाली उँगलियों से, उन हाथों से, छाती से और तिकोने जबड़े की घनी दाढ़ी से गुज़रकर मेरी नज़र उनकी झील जैसी आँखों में जा रुकी। तब पहली बार उन्होंने मुँह खोला।
‘‘बेटा, तुम इसी इलाक़े के हो ना ?’’
‘‘जी हाँ।’’
‘‘हिन्दू हो ?’’
‘‘हाँ।’’
‘‘बीबियों और देवियों की कहानियों की खोज में निकले हो ?’’
‘‘हाँ, हाँ वही।’’
‘‘हमारे देश में सैकड़ों ऐसी कहानियाँ भुला दी गई हैं। सुनना चाहोगे ?’’
‘‘हाँ-हाँ, बिलकुल।’’
जिस आदमी की उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, उसके अद्भुत ज्ञान के संबंध में मुझे कोई संदेह नहीं हुआ। देश के विभिन्न इलाक़ों की दंत कथाओं और जनश्रुतियों की खोज में निकला मैं मालिक के पास बैठे आज्ञाकारी कुत्ते की तरह, आदर के साथ, उस बूढ़े बाबा से चिपककर बैठ गया।
‘‘बेटा, जानते हो इस बीबी की कौन-सी बारी है ?’’
‘‘नहीं।’’
‘‘यह हमारे देश के तीसरी बीबी है। और भी न जाने कितने देवी-देवता इस देश में हुए हैं। इनके अलावा कई औलिया भी हैं। सबकी अपनी-अपनी दंत कथाएँ हैं। ये सब किसकी संपदा हैं ?’’
‘‘क्यों ? हम सबकी।’’
‘‘तुमने सही कहा। सारे-के-सारे देवी-देवता, औलिया और बीबियाँ सबके सब हमारे अपने हैं। जिस तरह ये बीबियाँ, बेटा तुम्हारी हैं यद्यपि हिन्दू हो, उसी तरह ये देवी-देवता मेरे भी हैं, यद्यपि मैं मुसलमान हूँ।’’
‘‘पहली बीबी तुम्हारे समुदाय की थी। जी हाँ, वह एक हिन्दू नायर खानदान की औरत थी। मेलेप्पुल्लारा ख़ानदान के बारे में सुना है ? आज उस खानदान में कोई भी ज़िन्दा नहीं। उसका विनाश हो गया। अच्छा, वह कहानी मैं तुम्हें सुना देता हूँ।’’
किसी विस्तृत मंत्र-ध्वनी की तरह उस ख़ानदान का नाम मेरे अंदर गूँज उठा। विश्व कथाकार ऋषि के साये में जैसे, मैं उस कहानी में विलीन हुआ। उनके शब्द तस्वीर बन प्रवाहित होने लगे। मेलेप्पुल्लारा हवेली की ओर जानेवाली लाल मिट्टी की चक्करदार सड़क दृश्यमान हो गई। बाबा की झील-सी आँखें और दाढ़ी के उलझे हुए सफ़ेद बाल सबकी गवाही देते प्रतीत हो रहे थे।
दो
कुहराच्छादित आकाश की नीलिमा की ओर हाथ जोड़कर मेलेप्पुल्लारा हवेली शान से खड़ी थी। प्रकृति और आसमान उत्सुकता में स्तब्ध थे। आधी रात की इस घड़ी में भी हवेली के अंदर से भरपूर पीला प्रकाश बाहर की ओर उछल रहा था।
रात को झकझोरते हुए एक नवजात शिशु का रोना निचली मंज़िल के उत्तरवाले एक कमरे से लगातार मुखरित होने लगा। वह प्रसूतिवाला कमरा था। दर्द से छुटकारा पाकर अम्मालू ने चैन की करवट बदली और अपनी बच्ची का स्पर्श पाया। ख़बर फैली कि लड़की हुई है और एक नई उर्वरता की ओर हवेली जाग उठी। अच्छा हुआ, पीढ़ियों का सातत्य नहीं रुका।
कमरे का दरवाजा धीरे से खोलकर अम्मालू की माँ ने दमदार आवाज़ में पूछा, ‘‘शंकू को ख़बर दी है न कि लड़की ही पैदा हुई है ?’’
ज्यों ही जीवन की पुकार ने धरती को छुआ, शंकू मेनोन ने समय की गणना के लिए सुराखवाली नारियल की खोपड़ी को पानी में बहा दिया था। आधी रात को शिशु का जन्म हुआ है। सूर्योदय के हिसाब से समय की सही गणना होनी चाहिए। ऐसे समय पर, जबकि सब निश्चिंत होने लगे कि उत्तारधिकारी के अभाव में मेलेप्पुल्लारा ख़ानदान का विनाश निश्चित है, बीजों को स्वीकार कर परंपरा को आगे बढ़ानेवाली लड़की का जन्म हुआ है। ग्रहों के स्थान के हिसाब से राशि निश्चित करने के लिए कुंडली बनाई जाएगी। पता नहीं ग्रहों के विन्यास ने शिशु के भाग्य में क्या-क्या लिख रखा है।
शंकु मेनोन ने राशि-चक्रों के आधार पर बच्ची के भविष्य की बातें जानने के लिए बेचैन अपनी उँगलियों को सँभाल लिया। निर्णय हो चुका है। आशंका और आकांक्षा से कोई फ़र्क नहीं पड़नेवाला। दीये की भरपूर रोशनी कमरे में फैल रही थी। हर बार जब जल घड़ीवाली खोपड़ी पानी में डूबी, मेनोन ने चावल का एक दाना अलग रखा और खोपड़ी को दुबारा जल के ऊपर छोड़ा। सपनों के प्रवाह के साथ बहकर देखो, रात की लंबाई मालूम नहीं होती। लेकिन घड़ी की इकाइयों में नाप लेते रहो, तभी पता चलता है कि रात कितनी लंबी होती है। कभी-कभी समय भी कितना असहनीय बन जाता है।
आख़िर युग की चाल से सरककर रात ढल गई और प्रातःकालीन तारे का उदय हुआ तो शंकू मेनोन उठ बैठे। जलघड़ीवाली नारियल की खोपड़ी को निकालकर दोनों की गिनती ली। उस रात को मेलेप्पुल्लारा हवेली ने पलकें नहीं झपकाई थीं। माँ और अन्य रिश्तेदारों का उद्वेग देखकर उन्होंने कहा, ‘‘मैंने सिर्फ़ समय का पता लगाया है। राशि-चक्र या कुंडली नहीं बनाई। वैसे भी परेशान होने से क्या फ़ायदा ? उससे बच्ची की तक़दीर तो नहीं बदलेगी ?’’
मन को एकाग्र करने की कोशिश करके मेनोन हार गए। कभी खेतों से निकलते झींगुरों के गीतों की ओर कभी लगातार कानों के पर्दों पर टकराते सियारों के हुआने की ओर उनका ध्यान बरबस खिंच जाता था। बंदर की तरह चंचल होते मन को बाँधने में असमर्थ होने के कारण राशि-चक्र तय करके बच्ची के भविष्य के बारे में विचार करने का साहस वे नहीं कर पाए।
रात को झकझोरते हुए एक नवजात शिशु का रोना निचली मंज़िल के उत्तरवाले एक कमरे से लगातार मुखरित होने लगा। वह प्रसूतिवाला कमरा था। दर्द से छुटकारा पाकर अम्मालू ने चैन की करवट बदली और अपनी बच्ची का स्पर्श पाया। ख़बर फैली कि लड़की हुई है और एक नई उर्वरता की ओर हवेली जाग उठी। अच्छा हुआ, पीढ़ियों का सातत्य नहीं रुका।
कमरे का दरवाजा धीरे से खोलकर अम्मालू की माँ ने दमदार आवाज़ में पूछा, ‘‘शंकू को ख़बर दी है न कि लड़की ही पैदा हुई है ?’’
ज्यों ही जीवन की पुकार ने धरती को छुआ, शंकू मेनोन ने समय की गणना के लिए सुराखवाली नारियल की खोपड़ी को पानी में बहा दिया था। आधी रात को शिशु का जन्म हुआ है। सूर्योदय के हिसाब से समय की सही गणना होनी चाहिए। ऐसे समय पर, जबकि सब निश्चिंत होने लगे कि उत्तारधिकारी के अभाव में मेलेप्पुल्लारा ख़ानदान का विनाश निश्चित है, बीजों को स्वीकार कर परंपरा को आगे बढ़ानेवाली लड़की का जन्म हुआ है। ग्रहों के स्थान के हिसाब से राशि निश्चित करने के लिए कुंडली बनाई जाएगी। पता नहीं ग्रहों के विन्यास ने शिशु के भाग्य में क्या-क्या लिख रखा है।
शंकु मेनोन ने राशि-चक्रों के आधार पर बच्ची के भविष्य की बातें जानने के लिए बेचैन अपनी उँगलियों को सँभाल लिया। निर्णय हो चुका है। आशंका और आकांक्षा से कोई फ़र्क नहीं पड़नेवाला। दीये की भरपूर रोशनी कमरे में फैल रही थी। हर बार जब जल घड़ीवाली खोपड़ी पानी में डूबी, मेनोन ने चावल का एक दाना अलग रखा और खोपड़ी को दुबारा जल के ऊपर छोड़ा। सपनों के प्रवाह के साथ बहकर देखो, रात की लंबाई मालूम नहीं होती। लेकिन घड़ी की इकाइयों में नाप लेते रहो, तभी पता चलता है कि रात कितनी लंबी होती है। कभी-कभी समय भी कितना असहनीय बन जाता है।
आख़िर युग की चाल से सरककर रात ढल गई और प्रातःकालीन तारे का उदय हुआ तो शंकू मेनोन उठ बैठे। जलघड़ीवाली नारियल की खोपड़ी को निकालकर दोनों की गिनती ली। उस रात को मेलेप्पुल्लारा हवेली ने पलकें नहीं झपकाई थीं। माँ और अन्य रिश्तेदारों का उद्वेग देखकर उन्होंने कहा, ‘‘मैंने सिर्फ़ समय का पता लगाया है। राशि-चक्र या कुंडली नहीं बनाई। वैसे भी परेशान होने से क्या फ़ायदा ? उससे बच्ची की तक़दीर तो नहीं बदलेगी ?’’
मन को एकाग्र करने की कोशिश करके मेनोन हार गए। कभी खेतों से निकलते झींगुरों के गीतों की ओर कभी लगातार कानों के पर्दों पर टकराते सियारों के हुआने की ओर उनका ध्यान बरबस खिंच जाता था। बंदर की तरह चंचल होते मन को बाँधने में असमर्थ होने के कारण राशि-चक्र तय करके बच्ची के भविष्य के बारे में विचार करने का साहस वे नहीं कर पाए।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book