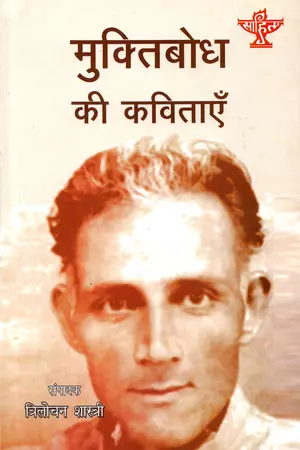|
कविता संग्रह >> मुक्तिबोध की कविताएँ मुक्तिबोध की कविताएँत्रिलोचन शास्त्री
|
277 पाठक हैं |
|||||||
मुक्तिबोध की कविताओं का मुख्य विशेषता उनकी भावुकता, गहराई और सांवेदनिकता है, जो उन्हें एक अनोखे स्थान पर रखती हैं। उनके काव्य में विशेष ध्यान भाषा की सुंदरता और शब्दचय के उपयोग पर दिया गया है, जो उनके काव्य को और भी मनोहारी बनाता है।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्रस्तुत संकलन में मुक्तिबोध की प्रतिनिधि कविताओं का चयन हिन्दी के प्रख्यात कवि त्रिलोकन शास्त्री से किया है जो भारतीय काव्य-जगत के सुपरिचित हस्ताक्षर हैं। आपकी कई कृतियाँ प्रकाशित हैं। ताप के ताए हुए दिन के लिए आप 1980 के साहित्य अकादेमी पुरस्कार तथा काव्य-साधना एवं सर्जना के लिए करीब सम्मान से अलंकृत हो चुके हैं।
भूमिका
मुक्तिबोध की कविताएं 1935 से पत्र-पत्रिकाओं में छपी हुई मिलती हैं और इन कविताओं के नीचे मूल कॉपियों के अभाव में उनका कविता लिखने का आरंभिक साल 1930 तक माना जा सकता है। यानी कविताएँ लिखना उन्होंने तभी शुरू किया होगा और कविताओं के बाद तारीख़ देने आदि की आदत किसी बड़ी उम्र के कवि की देखादेखी पड़ी होगी। उनके जीवन का यह काल जो उनके लेखन का आरंभिक काल भी है उनके परिचित साहित्यकारों के विवरणों में नहीं मिलता।
उन्हें जानने वाले जो आज भी हैं वे भी इस बात का विवरण नहीं दे पाते। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक विष्णुचन्द्र शर्मा भी उनके निर्माण काल के विषय में आवश्यक विवरण प्रमाण सहित नहीं दे पाए। इस कारण मुक्तिबोध के जीवन संबंधी तथ्य बहुत छिपे ही रह गये। उनके लेखन काल के आरंभिक साथियों ने भी इस दृष्टि से कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया। मुक्तिबोध रचनावली के दो संस्करण प्रकाशित हैं जिसमें उनकी कविताएं, कहानियाँ, समीक्षाएँ आदि विषयानुकूल विभाजन द्वारा संकलित की गयी हैं, उनका लिखा हुआ जो भी साहित्य उपलब्ध हुआ वह उनके दीर्घकालीन मित्र और रचनावली के संपादक नेमिचन्द्र जैन ने संकलित किया है। प्रायः रचनाओं का काल आनुमानिक है। ध्यान से पढ़ने पर यही बात सिद्ध होती है। मुक्तिबोध की आत्मकथा में लेखक विष्णुचन्द्र शर्मा ने भरसक उपलब्ध तथ्यों का संकलन करते हुए आत्मकथा की शैली में मुक्तिबोध की जीवनी प्रस्तुत की है। यह किताब मुक्तिबोध के विषय में अध्ययन करनेवालों के लिए अनिवार्य रहेगी।
कविता का आरंभ बड़ी जटिल परिस्थितियों में हुआ करता है। उसको इदम् इत्थम के ढंग पर नहीं बताया जा सकता कभी-कभी चित्तवृत्तियों के प्रभाव से ही कविताओं का रूप निर्धारण होता है। ये कविताएँ व्यवस्थित छंदों या नाना रूपात्मक मुक्त छंदों में हो सकती हैं। छन्द और मुक्त छंद दोंनों में छंद समावेश है। व्यवस्थित छंद में अनुशासित लय का प्रयोग हर चरण में किया जाता है। मुक्त छंद में चरण का महत्त्व नहीं होता। वहाँ भाव-भाषा की ईकाई के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। भाषा की इकाई वाक्य ही है। यह इकाई, जो मुक्त छंद द्वारा रखी जाती है, मूल छंद की आंतरिक लय को कहीं आहत नहीं करती। जो समान नाप-तोल की पंक्तियों को ही यानी विभिन्न छंदों की ही कविता के लिए अनिवार्य मानते हैं वे मुक्त छंद को अच्छी तरह समझ नहीं पाते। हिन्दी में मुक्त छंद के नाम पर ऐसी कविताएँ बहुत लिखी गई हैं जिनमें छंद का कोई भी तत्त्व कहीं नहीं है। छंद के अलावा भाषाई सुंदरता की पहचान भी सर्वसुलभ नहीं हो पाती। भाषायी सुंदरता पहचानने वाली आँखें अधिक नहीं मिलती। फिर भी जीवन के संबंध में कोई विवरण जब कहा जाता है तब तथ्य के ही आधार पर उसकी वस्तुगत और विषयगत परीक्षा की जाती है।
सन् 1930 से हिन्दी में छायावाद को स्वीकार करने वालों की संख्या युवा पीढ़ी में बहुत बढ़ गयी थी। ब्रजभाषा कविता के समर्थक 31 से 40 वाले दशाब्द में उत्तरोत्तर कम होते गये। ब्रजभाषा ही कविता के लिए उपयुक्त है इस सिद्धान्त के समर्थक कवि और विद्वान धीरे-धीरे अल्पतम हो गये। छायावादी कवियों ने आधुनिक हिंदी में लिखी जानेवाली कविताओं को वह ऊँचाई दी जिससे हिंदी कविता किसी भी भाषा की कविता से न्यून नहीं रह गयी। धीरे-धीरे आधुनिक हिंदी काव्य के लिए उपयुक्त माध्यम स्वीकार किया कर ली गयी।
मुक्तिबोध उस पीढ़ी के कवियों में एक है जिसका जन्मकाल 1911 से 1920 तक है। इस पीढ़ी की काव्य शिक्षा छायावादी कविता द्वारा पूरी हुई। छंद, व्यंजना और विषय यह सब छायावादी कविता के प्रभाव से ही बदले। इस पीढ़ी के कवियों ने अन्य देशों की कविताओं के अंग्रेजी में अनुवाद भी पढ़े और उनका ज्ञान का क्षितिज उत्तरोत्तर बढ़ता गया। ब्रजभाषा कविता का संचारी और स्थायी भाव नये कवियों के लिए आवश्यक नहीं रह गया। परिणामतः कविता बिना घोषणा किए रूप और आकार में बदलती गयी।
मुक्तिबोध का जन्म 13 नवम्बर 1917 को श्योपुर, ग्वालियर में हुआ। उनके पिता रियासत (ग्वालियर) की पुलिस सेवा में थे। जहाँ-जहाँ भी उनका स्थानान्तरण होता था उनका परिवार भी साथ ही जाता था। इस तरह उनकी शिक्षा के स्थान भी बदलते रहे। घर की मराठी और घर के बाहर तथा स्कूल की भाषा हिंदी थी। घरेलू वातावरण भी हिंदी से अछूता न था। इनकी माँ प्रेमचन्द आदि का साहित्य पढ़ा करती थीं और माँ की पढ़ी हुई पुस्तकें मुक्तिबोध भी पढते थे। मुक्तिबोध ने हिन्दी कविता का अध्ययन बड़े व्यापक रूप में किया था। उनको मानसिक विश्राम छायावादी कवियों के बाद अपनी समकालिक कविता में ही मिलता था। अपने समकालिक कवियों पर उन्होंने जहाँ-तहाँ अपने विचार लिखे भी हैं। आधुनिक हिंदी कविताएं पढ़ते-पढ़ते मुक्तिबोध ने जो कविताएं प्रकाशित करायीं उन कविताओं पर मध्य भारतीय लेखकों और कवियों का असर भी देखा जा सकता है।
हिंदी की कविता में 1931 से 40 के मध्य एक परिवर्तन धीरे-धीरे प्रकट हो रहा था जो इसी अरसे में छायावाद की कविता से कुछ भिन्न था। इस परिवर्तन का प्रभाव उन कवियों से प्रकट हो रहा था जो अंग्रेजी की नयी कविता के अत्यंत परिचित और प्रभावित थे। इसी कारण इन कवियों की कविताओं में छायावाद की कविता से भिन्नता मिलती है। ये सभी कवि छायावादी कवियों को भी पढ़ते थे साथ ही जानी-पहचानी अन्य भाषाओं की कविताओं को भी पढ़ते थे। इस प्रकार इनके द्वारा शैली और विषय में परिवर्तन आना अनिवार्य था। 1943 में हिंदी के सात कवियों का एक संकलन ‘तारसप्तक’ नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें संगृहित कवि इस प्रकार हैं- गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिराज माथुर, नेमिचन्द्र जैन, प्रभाकर माचवे, भारतभूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा और सच्चिदानंद हीरानन्द वात्स्यायन ‘अज्ञेय’।
इस संग्रह के संपादक की हैसियत से अज्ञेय ने इन सभी कवियों को ‘राहों का अन्वेषी’ कहा था। हर कवि की कविता के विषय में उनका आत्मवक्तव्य इस संकलन में था। इस प्रकार का कोई संकलन इसके पहले हिंदी में नहीं था। द्विवेदी युग में ‘काव्य-कलाप’ नाम से पाँच कवियों की कविताओं का संकलन निकला था जिसका संपादन महावीरप्रसाद द्विवेदी ने किया था। इसके बाद सन् 1937 के आसपास तीन कवियों का एक संकलन निकाला था जिसका नाम था ‘त्रिधारा’। ‘त्रिधारा’ में तीन कवि थे- माखनलाल चतुर्वेदी सुभद्राकुमारी चौहान और केशवप्रसाद पाठक। ‘काव्य-कलाप’ और ‘त्रिधारा’ में तारसप्तक के कवियों की तरह दावे नहीं किये गये थे। ‘तारसप्तक’ पर समीक्षकों ने काफी दिनों ध्यान नहीं दिया। इस पर पहली समीक्षा नया-साहित्य (बम्बई) ने 1947 में छापी थी। समीक्षक थे शमशेर बहादुर सिंह। इस समीक्षा में अज्ञेय, रामविलास शर्मा गिरिजाकुमार माथुर आदि की कविताओं पर ध्यान दिया गया था और जिन कवियों को यूँ ही चालू कर दिया जाता था। उन्हीं में गजानन माधव मुक्तिबोध भी थे।
1964 में ‘चाँद’ का मुँह टेढ़ा है’ उनकी लंबी कविताओं का एक संकलन निकला है। प्रकाशित होने के कुछ पूर्व की कवि का देहावसान हो चुका था। उनके प्रथम संग्रह की भूमिका श्रीकांत वर्मा और शमशेरबहादुर सिंह ने लिखी थी। इसके बाद उनकी कविताओं का एक संकलन ‘भूरी-भूरी खाक धूलि’ शीर्षक से प्रकाशित हुआ। नयी हिंदी कविता की चर्चा के समय मुक्तिबोध का नाम प्रथमस्तरीय हो गया है। मुक्तिबोध के पूरे काव्य को ध्यान में रखते हुए उनकी कविताओं को तीन काल खंडों में बाँट सकते हैं- 1935 से 1947, 1948 से 1955 और 1956 से 1963 तक। पहले कालखंड की कविताएँ इतर कवियों से बहुत भिन्न नहीं हैं। इस कालखंड की कविताएं अंतिम कालखंड की कविताओं अथवा बीचवाले कालखंड वाली कविताओं से यत्र-तत्र मेल दिखा देती हैं। 1956 से 1963 तक की कविताओं का दौर उनकी दीर्घतम कविताओं का दौर है। अंतिम आठ वर्षों में मुक्तिबोध ने पहली लिखी हुई कविताओं में भी संशोधन और परिवर्धन इसी काल में किया गया है। उनके विचारात्मक निबंध भी इसी दौर के हैं।
रचना की दृष्टि से जो ये तीन विभाजन किये जा रहे हैं इसका मतलब नहीं है कि उनका कोई कालखंड ऐसा भी है जो ध्यान देने योग्य नहीं है। 1935 से 1947 तक के कालखंड की कविताएँ बहुत भिन्न न होते हुए भी इसी पहले कालखंड में मिलती हैं। व्यवस्थित छंदों की आंतरिक लय का प्रयोग 1956 वाले कालखंड में भी मिल जाता है। लेकिन अंतिम कालखंड रचना कौशल और काव्य-भाषा की दृष्टि से ज्यादा परिपक्व है। पहले कालखंड में माखनलाल चतुर्वेदी, पंत आदि हिंदी कवियों की कविताओं के असर उन पर हैं। क्रमशः वह प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े और प्रगतिशील लेखक संघ के लिए भी उन्होंने अधिवेशन किए। इसके बाद वे जहाँ कहीं रहे बराबर प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े रहे। उन्होंने निबंधों की तुलना पर किये जाने वाले प्रहारों के उत्तर-रूप में लिखे। सभी निबंधों में उन्होंने अपने को प्रगतिशील और मार्क्सवादी कहा है। फिर भी कुछ आलोचक उन्हें मार्क्सवादी नहीं मानते। इस पर इतना ही कहा जा सकता है कि मुक्तिबोध की मार्क्सवाद की धारणा औरों से वैसे ही भिन्न है जैसे बहुत-से रूसी समीक्षकों और चिन्तकों की आपस में भिन्न दिखाई देती है। मूल सिद्धान्त एक होते हुए भी समझने-समझाने और आचरण करने में समय और परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति- भेद भिन्नता आ सकती है।
मुक्तिबोध की कविताएँ अन्य प्रगतिशील कवियों से अलग होते हुए प्रगति विरोधी नहीं हैं। मुक्तिबोध के निबन्धों को ध्यान से पढ़ा जाय तो यह बात स्पष्ट हो जाती है। मुक्तिबोध हिंदी की प्रगतिशील समीक्षा से भी बहुत संतुष्ट नहीं थे। अतः उन्होंने प्रगतिशील समीक्षा के दोषों और अभावों पर बड़ी स्पष्टता से अपने निबन्धों में लिखा है। इस कारण उन्हें साहित्य संबंधी अपने विचार स्पष्ट रूप से लिखने पड़े।
उन्हें जानने वाले जो आज भी हैं वे भी इस बात का विवरण नहीं दे पाते। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक विष्णुचन्द्र शर्मा भी उनके निर्माण काल के विषय में आवश्यक विवरण प्रमाण सहित नहीं दे पाए। इस कारण मुक्तिबोध के जीवन संबंधी तथ्य बहुत छिपे ही रह गये। उनके लेखन काल के आरंभिक साथियों ने भी इस दृष्टि से कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया। मुक्तिबोध रचनावली के दो संस्करण प्रकाशित हैं जिसमें उनकी कविताएं, कहानियाँ, समीक्षाएँ आदि विषयानुकूल विभाजन द्वारा संकलित की गयी हैं, उनका लिखा हुआ जो भी साहित्य उपलब्ध हुआ वह उनके दीर्घकालीन मित्र और रचनावली के संपादक नेमिचन्द्र जैन ने संकलित किया है। प्रायः रचनाओं का काल आनुमानिक है। ध्यान से पढ़ने पर यही बात सिद्ध होती है। मुक्तिबोध की आत्मकथा में लेखक विष्णुचन्द्र शर्मा ने भरसक उपलब्ध तथ्यों का संकलन करते हुए आत्मकथा की शैली में मुक्तिबोध की जीवनी प्रस्तुत की है। यह किताब मुक्तिबोध के विषय में अध्ययन करनेवालों के लिए अनिवार्य रहेगी।
कविता का आरंभ बड़ी जटिल परिस्थितियों में हुआ करता है। उसको इदम् इत्थम के ढंग पर नहीं बताया जा सकता कभी-कभी चित्तवृत्तियों के प्रभाव से ही कविताओं का रूप निर्धारण होता है। ये कविताएँ व्यवस्थित छंदों या नाना रूपात्मक मुक्त छंदों में हो सकती हैं। छन्द और मुक्त छंद दोंनों में छंद समावेश है। व्यवस्थित छंद में अनुशासित लय का प्रयोग हर चरण में किया जाता है। मुक्त छंद में चरण का महत्त्व नहीं होता। वहाँ भाव-भाषा की ईकाई के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। भाषा की इकाई वाक्य ही है। यह इकाई, जो मुक्त छंद द्वारा रखी जाती है, मूल छंद की आंतरिक लय को कहीं आहत नहीं करती। जो समान नाप-तोल की पंक्तियों को ही यानी विभिन्न छंदों की ही कविता के लिए अनिवार्य मानते हैं वे मुक्त छंद को अच्छी तरह समझ नहीं पाते। हिन्दी में मुक्त छंद के नाम पर ऐसी कविताएँ बहुत लिखी गई हैं जिनमें छंद का कोई भी तत्त्व कहीं नहीं है। छंद के अलावा भाषाई सुंदरता की पहचान भी सर्वसुलभ नहीं हो पाती। भाषायी सुंदरता पहचानने वाली आँखें अधिक नहीं मिलती। फिर भी जीवन के संबंध में कोई विवरण जब कहा जाता है तब तथ्य के ही आधार पर उसकी वस्तुगत और विषयगत परीक्षा की जाती है।
सन् 1930 से हिन्दी में छायावाद को स्वीकार करने वालों की संख्या युवा पीढ़ी में बहुत बढ़ गयी थी। ब्रजभाषा कविता के समर्थक 31 से 40 वाले दशाब्द में उत्तरोत्तर कम होते गये। ब्रजभाषा ही कविता के लिए उपयुक्त है इस सिद्धान्त के समर्थक कवि और विद्वान धीरे-धीरे अल्पतम हो गये। छायावादी कवियों ने आधुनिक हिंदी में लिखी जानेवाली कविताओं को वह ऊँचाई दी जिससे हिंदी कविता किसी भी भाषा की कविता से न्यून नहीं रह गयी। धीरे-धीरे आधुनिक हिंदी काव्य के लिए उपयुक्त माध्यम स्वीकार किया कर ली गयी।
मुक्तिबोध उस पीढ़ी के कवियों में एक है जिसका जन्मकाल 1911 से 1920 तक है। इस पीढ़ी की काव्य शिक्षा छायावादी कविता द्वारा पूरी हुई। छंद, व्यंजना और विषय यह सब छायावादी कविता के प्रभाव से ही बदले। इस पीढ़ी के कवियों ने अन्य देशों की कविताओं के अंग्रेजी में अनुवाद भी पढ़े और उनका ज्ञान का क्षितिज उत्तरोत्तर बढ़ता गया। ब्रजभाषा कविता का संचारी और स्थायी भाव नये कवियों के लिए आवश्यक नहीं रह गया। परिणामतः कविता बिना घोषणा किए रूप और आकार में बदलती गयी।
मुक्तिबोध का जन्म 13 नवम्बर 1917 को श्योपुर, ग्वालियर में हुआ। उनके पिता रियासत (ग्वालियर) की पुलिस सेवा में थे। जहाँ-जहाँ भी उनका स्थानान्तरण होता था उनका परिवार भी साथ ही जाता था। इस तरह उनकी शिक्षा के स्थान भी बदलते रहे। घर की मराठी और घर के बाहर तथा स्कूल की भाषा हिंदी थी। घरेलू वातावरण भी हिंदी से अछूता न था। इनकी माँ प्रेमचन्द आदि का साहित्य पढ़ा करती थीं और माँ की पढ़ी हुई पुस्तकें मुक्तिबोध भी पढते थे। मुक्तिबोध ने हिन्दी कविता का अध्ययन बड़े व्यापक रूप में किया था। उनको मानसिक विश्राम छायावादी कवियों के बाद अपनी समकालिक कविता में ही मिलता था। अपने समकालिक कवियों पर उन्होंने जहाँ-तहाँ अपने विचार लिखे भी हैं। आधुनिक हिंदी कविताएं पढ़ते-पढ़ते मुक्तिबोध ने जो कविताएं प्रकाशित करायीं उन कविताओं पर मध्य भारतीय लेखकों और कवियों का असर भी देखा जा सकता है।
हिंदी की कविता में 1931 से 40 के मध्य एक परिवर्तन धीरे-धीरे प्रकट हो रहा था जो इसी अरसे में छायावाद की कविता से कुछ भिन्न था। इस परिवर्तन का प्रभाव उन कवियों से प्रकट हो रहा था जो अंग्रेजी की नयी कविता के अत्यंत परिचित और प्रभावित थे। इसी कारण इन कवियों की कविताओं में छायावाद की कविता से भिन्नता मिलती है। ये सभी कवि छायावादी कवियों को भी पढ़ते थे साथ ही जानी-पहचानी अन्य भाषाओं की कविताओं को भी पढ़ते थे। इस प्रकार इनके द्वारा शैली और विषय में परिवर्तन आना अनिवार्य था। 1943 में हिंदी के सात कवियों का एक संकलन ‘तारसप्तक’ नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें संगृहित कवि इस प्रकार हैं- गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिराज माथुर, नेमिचन्द्र जैन, प्रभाकर माचवे, भारतभूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा और सच्चिदानंद हीरानन्द वात्स्यायन ‘अज्ञेय’।
इस संग्रह के संपादक की हैसियत से अज्ञेय ने इन सभी कवियों को ‘राहों का अन्वेषी’ कहा था। हर कवि की कविता के विषय में उनका आत्मवक्तव्य इस संकलन में था। इस प्रकार का कोई संकलन इसके पहले हिंदी में नहीं था। द्विवेदी युग में ‘काव्य-कलाप’ नाम से पाँच कवियों की कविताओं का संकलन निकला था जिसका संपादन महावीरप्रसाद द्विवेदी ने किया था। इसके बाद सन् 1937 के आसपास तीन कवियों का एक संकलन निकाला था जिसका नाम था ‘त्रिधारा’। ‘त्रिधारा’ में तीन कवि थे- माखनलाल चतुर्वेदी सुभद्राकुमारी चौहान और केशवप्रसाद पाठक। ‘काव्य-कलाप’ और ‘त्रिधारा’ में तारसप्तक के कवियों की तरह दावे नहीं किये गये थे। ‘तारसप्तक’ पर समीक्षकों ने काफी दिनों ध्यान नहीं दिया। इस पर पहली समीक्षा नया-साहित्य (बम्बई) ने 1947 में छापी थी। समीक्षक थे शमशेर बहादुर सिंह। इस समीक्षा में अज्ञेय, रामविलास शर्मा गिरिजाकुमार माथुर आदि की कविताओं पर ध्यान दिया गया था और जिन कवियों को यूँ ही चालू कर दिया जाता था। उन्हीं में गजानन माधव मुक्तिबोध भी थे।
1964 में ‘चाँद’ का मुँह टेढ़ा है’ उनकी लंबी कविताओं का एक संकलन निकला है। प्रकाशित होने के कुछ पूर्व की कवि का देहावसान हो चुका था। उनके प्रथम संग्रह की भूमिका श्रीकांत वर्मा और शमशेरबहादुर सिंह ने लिखी थी। इसके बाद उनकी कविताओं का एक संकलन ‘भूरी-भूरी खाक धूलि’ शीर्षक से प्रकाशित हुआ। नयी हिंदी कविता की चर्चा के समय मुक्तिबोध का नाम प्रथमस्तरीय हो गया है। मुक्तिबोध के पूरे काव्य को ध्यान में रखते हुए उनकी कविताओं को तीन काल खंडों में बाँट सकते हैं- 1935 से 1947, 1948 से 1955 और 1956 से 1963 तक। पहले कालखंड की कविताएँ इतर कवियों से बहुत भिन्न नहीं हैं। इस कालखंड की कविताएं अंतिम कालखंड की कविताओं अथवा बीचवाले कालखंड वाली कविताओं से यत्र-तत्र मेल दिखा देती हैं। 1956 से 1963 तक की कविताओं का दौर उनकी दीर्घतम कविताओं का दौर है। अंतिम आठ वर्षों में मुक्तिबोध ने पहली लिखी हुई कविताओं में भी संशोधन और परिवर्धन इसी काल में किया गया है। उनके विचारात्मक निबंध भी इसी दौर के हैं।
रचना की दृष्टि से जो ये तीन विभाजन किये जा रहे हैं इसका मतलब नहीं है कि उनका कोई कालखंड ऐसा भी है जो ध्यान देने योग्य नहीं है। 1935 से 1947 तक के कालखंड की कविताएँ बहुत भिन्न न होते हुए भी इसी पहले कालखंड में मिलती हैं। व्यवस्थित छंदों की आंतरिक लय का प्रयोग 1956 वाले कालखंड में भी मिल जाता है। लेकिन अंतिम कालखंड रचना कौशल और काव्य-भाषा की दृष्टि से ज्यादा परिपक्व है। पहले कालखंड में माखनलाल चतुर्वेदी, पंत आदि हिंदी कवियों की कविताओं के असर उन पर हैं। क्रमशः वह प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े और प्रगतिशील लेखक संघ के लिए भी उन्होंने अधिवेशन किए। इसके बाद वे जहाँ कहीं रहे बराबर प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े रहे। उन्होंने निबंधों की तुलना पर किये जाने वाले प्रहारों के उत्तर-रूप में लिखे। सभी निबंधों में उन्होंने अपने को प्रगतिशील और मार्क्सवादी कहा है। फिर भी कुछ आलोचक उन्हें मार्क्सवादी नहीं मानते। इस पर इतना ही कहा जा सकता है कि मुक्तिबोध की मार्क्सवाद की धारणा औरों से वैसे ही भिन्न है जैसे बहुत-से रूसी समीक्षकों और चिन्तकों की आपस में भिन्न दिखाई देती है। मूल सिद्धान्त एक होते हुए भी समझने-समझाने और आचरण करने में समय और परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति- भेद भिन्नता आ सकती है।
मुक्तिबोध की कविताएँ अन्य प्रगतिशील कवियों से अलग होते हुए प्रगति विरोधी नहीं हैं। मुक्तिबोध के निबन्धों को ध्यान से पढ़ा जाय तो यह बात स्पष्ट हो जाती है। मुक्तिबोध हिंदी की प्रगतिशील समीक्षा से भी बहुत संतुष्ट नहीं थे। अतः उन्होंने प्रगतिशील समीक्षा के दोषों और अभावों पर बड़ी स्पष्टता से अपने निबन्धों में लिखा है। इस कारण उन्हें साहित्य संबंधी अपने विचार स्पष्ट रूप से लिखने पड़े।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book