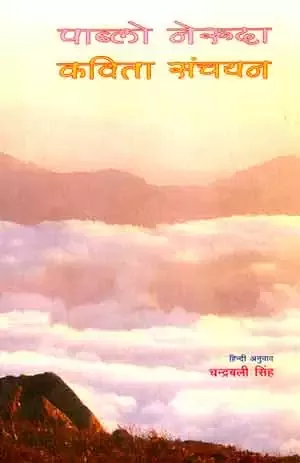|
कविता संग्रह >> पाब्लो नेरूदा कविता संचयन पाब्लो नेरूदा कविता संचयनचन्द्रबली सिंह
|
425 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत काव्य संचयन में पाब्लो नेरुदा की सर्वश्रेष्ठ कविताएँ
Palbo Neruda Kavita Sanchayan
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
पाब्लो नेरूदा की कृतियों में आइला नेग्रा, ह्वेयर द रेन इज बोर्न, द मून इन द लेबिरिन्थ क्रूएल, द हंटर आफ्टर रूट्स क्रिटिकल सोनाटा, और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ट्वेन्टी लव पोएम्स एंड द सांग ऑफ़ डेस्पेयर की करोड़ों प्रतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी लगभग सभी रचनाएँ विश्व की बीस से भी अधिक प्रमुख भाषाओं में अनूदित हो चुकी है। एक यशस्वी कवि के तौर पर अपने पाठकों के बीच पर्याप्त समादृत हो चुके नेरूदा के नौ काव्य-संग्रह उनके मरणोपरान्त प्रकाशित हुए और हाथोंहाथ बिक गए।
पाब्लो नेरूदा का लक्ष्य था, स्पैनिश कविता को उन्नीसवीं शताब्दी की साहित्यिक आलोचनाओं से निकालकर उसे अकृत्रिम पहचान देना और साथ ही बीसवीं शताब्दी की सुपरिचित लयात्मक शैली में स्थापित करना। उन्होंने अपनी मृत्यु के एकदम पहले लिखे एक संस्मरण में स्वयं को इस बात का श्रेय भी दिया कि उन्होंने अपने पुनर्संधान द्वारा कविता को सम्माननीय स्थान दिलवाया और विश्व कविता के समक्ष निश्चय ही एक नया प्रतिमान प्रस्तुत किया। उनकी कृतियाँ एक ओर जहाँ महाद्वीपों के स्त्री-पुरुषों द्वारा व्यक्त की गई स्थानीय आकांक्षाओं और उनसे जुड़ी नियति का सच्चा प्रतिनिधित्व करती हैं वहीं दूसरी ओर समस्त विश्व की मानवीय संवेदनाओं का सम्मान करती हैं-क्योंकि कोई भी सच्ची कृति प्रदत्त और प्राप्तव्य विश्व की अनदेखी नहीं कर सकती।
प्रस्तुत काव्य संचयन पाब्लो नेरूदा के जन्मशती वर्ष में साहित्य अकादेमी की विनम्र श्रद्धांजलि है
पाब्लो नेरूदा का लक्ष्य था, स्पैनिश कविता को उन्नीसवीं शताब्दी की साहित्यिक आलोचनाओं से निकालकर उसे अकृत्रिम पहचान देना और साथ ही बीसवीं शताब्दी की सुपरिचित लयात्मक शैली में स्थापित करना। उन्होंने अपनी मृत्यु के एकदम पहले लिखे एक संस्मरण में स्वयं को इस बात का श्रेय भी दिया कि उन्होंने अपने पुनर्संधान द्वारा कविता को सम्माननीय स्थान दिलवाया और विश्व कविता के समक्ष निश्चय ही एक नया प्रतिमान प्रस्तुत किया। उनकी कृतियाँ एक ओर जहाँ महाद्वीपों के स्त्री-पुरुषों द्वारा व्यक्त की गई स्थानीय आकांक्षाओं और उनसे जुड़ी नियति का सच्चा प्रतिनिधित्व करती हैं वहीं दूसरी ओर समस्त विश्व की मानवीय संवेदनाओं का सम्मान करती हैं-क्योंकि कोई भी सच्ची कृति प्रदत्त और प्राप्तव्य विश्व की अनदेखी नहीं कर सकती।
प्रस्तुत काव्य संचयन पाब्लो नेरूदा के जन्मशती वर्ष में साहित्य अकादेमी की विनम्र श्रद्धांजलि है
पृथ्वी का कवि पाब्लो नेरूदा
पाब्लो नेरुदा की कविताओं में यह हिन्दी संचयन कवि की तीसवीं बरसी पर एक विनम्र श्रद्धांजलि है और जन्मशती के उपलक्ष्य में अग्रिम उपहार भी। ऐसे काव्यात्मक स्तबक के लिए हिन्दी जगत अपने वरिष्ठ जनवादी समालोचक चन्द्रबली सिंह के प्रति कृतज्ञ रहेगा।
नेरुदा मेरे भी प्रिय कवि हैं और उनकी कविताओं का हिन्दी अनुवाद करनेवाले डॉ. चन्द्रबली सिंह तो मेरे आदरणीय अग्रज ही हैं, इसलिए यहाँ कुछ कहने की हिमाकत कर रहा हूँ, वरना स्वयं अनुवादक की विस्तृत भूमिका के बाद कुछ भी कहना ग़ैरज़रूरी है। सबसे पहले तो यही है कि इस पुस्तक के प्रकाशन पर व्यक्तित्व रूप से मुझे जो आत्मसंतोष हुआ वह स्वयं अपनी किसी पुस्तक के प्रकाशन के समय भी नहीं हुआ। कारण यह है कि अनुवाद के उस कठिन जीवन-संघर्ष और आत्मसंघर्ष की गहरी पीड़ा को कुछ-कुछ निकट से देखने का मुझे अवसर मिला है। कोई भी दूसरा व्यक्ति उस संघर्ष में टूटकर बिखर सकता था। शायद यह अनुवाद कर्म की संजीवनी ही है जिसने उन्हें बचाए रखा और आज वे अपनी आँखों अपनी अनवरत साधना को फलीभूत देखने की स्थिति में हैं। वे पक्के परिपूर्णतावादी हैं इतने कि अन्तिम प्रूफ़ की अवस्था तक काट-छाँट, सुधार-सँवार की ज़िद पर अड़े रहे। मुकम्मल पांडुलिपि भी ‘किस तरह खैंच के लाया हूँ कि जी जानता है।’ कहना न होगा कि कविता-वह भी नेरुदा की कविता का अनुवाद चन्द्रबली सिंह के लिए कोई धन्धा नहीं बल्कि गहरी प्रतिबद्धता है।
‘शब्द ख़ून में पैदा होता है’ जैसा कि नेरुदा ने किसी कविता में कहा है और ‘शब्द ही ख़ून को ख़ून और ज़िन्दगी को ज़िन्दगी देते हैं। चन्द्रबली सिंह के इस भाषान्तर के बारे में भी यह बात उतनी ही सच है। उनके अनुवाद की रगों में भी ख़ून बहता दिखाई देता है जिसमें नेरूदा के ख़ून की गरमाहट है।
कुल मिलाकर, कविताओं का अनुवाद कैसा बन पड़ा है, यह तो वही बता सकते हैं जिन्होंने इस मैदान में हाथ आज़माए हैं। एक सामान्य पाठक के नाते सरसरी तौर पर फ़िलहाल मुझे यही लगता है कि स्पेनिश मूल से किए हुए अनुवादों से ये अनुवाद कई जगह हैं और अक्सर अंग्रेज़ी अनुवादों से टक्कर लेते हैं। यह ज़रूर है कि भाषा उतनी चलती हुई नहीं है बल्कि कुछ-कुछ किताबी-सी हो गई है। एक ‘माच्चु पिच्चु के शिखर’ कविता के विभिन्न हिन्दी अनुवादों की तुलना से यह स्पष्ट हो सकती है।
वैसे, ‘माच्चु पिच्चु के शिखर’ नेरुदा की कविता का शिखर भले ही हो, समूचा काव्य संसार नहीं है। इस शिखर के सम्मुख नतमस्तक मैं भी हूँ लेकिन नीचे की घाटियों में ऐसी अनेक जगह हैं। जो कहीं अधिक रम्य और मनोज्ञ हैं। यह विविधता और बहुलता ही नेरुदा की नेरुदा की कविता की प्रकृति है। नेरुदा इतने स्वरों और शैलियों में बोलते हैं कि उनकी कविता को किसी एक साँचे में कसना मुश्किल है। इस तरह ‘नेरुदावाद’ के पहले दुश्मन तो नेरुदा स्वयं हैं।
नेरुदा ने अपनी पचास वर्षों से भी अधिक लम्बी काव्य-यात्रा में कविता को इतनी बार बदला है कि कुछ लोग उन्हें ‘कविता का पिकासो’ कहते हैं।
उनमें किसी भी चीज़ या विषय पर कविता लिखने की असाधारण क्षमता थी। उनके लिए जिसका भी वजूद हो ऐसी हर चीज़ समान रूप से सम्मान के योग्य है और इस नाते वह कविता का विषय भी हो सकती है। कोई चाहे तो इसे कविता का विलक्षण ‘लोकतंत्र’ भी कह सकता है।
इसलिए नेरुदा ऐसी अनपेक्षित जगहों में भी कविता पा जाते थे जहाँ उनकी कोई सम्भावना नहीं होती। सम्भवतः इसी वजह से उनकी प्रत्येक कृति अप्रत्याशित की तरह आती थी। अपनी कविता में वे अक्सर ‘काल्पनिक’ और ‘वास्तविक’ के भेद को इतनी सहजता से मिटा देते हैं कि एक अलौकिक काव्यलोक निर्मित हो जाता है और आगे चलकर गार्सिया मारखेस ने यही काम ‘एकान्तवास के सौ साल’ नामक उपन्यास में किया तो उसे ‘जादुई यथार्थवाद’ का नाम दिया गया। कहना न होगा, इस जादुई यथार्थवाद का प्रयोग नेरुदा पहले ही कर चुके थे और वह भी कविता में। पर 1925 की लिखी उनकी प्रसिद्ध कविता ‘घूमते हुए’ को देखें तो उसमें परस्पर विरोधी और बेमेल बिम्ब इतनी तेज़ रफ़्तार से एक-के-बाद-एक आते हैं कि चकित रह जाना पड़ता है। कविता शुरू होती है इस तरह ‘ऐसा है कि मैं आदमी होने से थक गया हूँ’ और फिर कविता भी घूमते हुए आदमी की तरह ही घूमती रहती है।
सहसा यह पंक्ति आती है ‘जहाँ हड्डियाँ अस्पताल की खिड़कियों के बाहर उड़ती हैं’ और कुछ देर बाद ‘काफी के प्याले में छूट गए नक़ली दाँत’ दिखते हैं। यह एक प्रकार का ‘सुर्रियलज़्म’ यानी ‘अतियथार्थवाद’ है लेकिन जाने-माने ‘अतियथार्थवादियों’ से बिल्कुल अलग। वे अवचेतन के मारे’ सुर्रियलिस्ट’ नहीं, बल्कि अपने आस-पास के चिरपरिचित वातावरण के ‘अतियथार्थवादी’ रूप के ही सहज दर्शक हैं।
नेरुदा की इस तरह की दिलचस्प कविताओं का ज़िक्र इसलिए ज़रूरी है कि उनकी सामान्य छवि केवल एक ‘प्रतिबद्ध’ कम्युनिस्ट कवि की है, जबकि सचाई कुछ और ही है, नेरुदा की पहली कविता-पुस्तक ‘बीस प्रेम कविताएँ और निराशा का एक गीत’ है, जो 1924 में प्रकाशित हुई थी। उस समय नेरुदा बीस की वय के एक युवक थे। इसी कविता-संग्रह ने नेरुदा को सहसा यश के शिखर पर पहुँचा दिया था। कुछ लोग आज उस संग्रह की कविताओं को नेरुदा की सबसे अच्छी कविताओं में गिनते हैं। ‘लिख सकता हूँ सबसे उदास कविताएँ आज की रात’ जैसी लोकप्रिय कविता इसी संग्रह की है। प्रेम कविताओं का यह सिलसिला आगे भी चलता रहा, बल्कि अंतिम वर्षों में तो इस इलाके में बाढ़-सी आ गई। इस्ला नेग्रा (1964) का प्रथम संस्करण तो ‘मातिल्दे उर्रुतिया’ को समर्पित भी है और पूरा संकलन ही जैसे प्रेम पर एक प्रलम्बित अनुचिन्तन है।
नेरुदा प्रेम से भी अधिक काम के कवि हैं। वे उन कवियों में से हैं जो ‘सेक्स’ की वर्जना से सर्वथा मुक्त रहते हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि नेरुदा के लिए काव्य-सर्जना कामभावना का पर्याय जैसा है।
वैसे भी परम स्वच्छन्द नेरुदा सभी प्रकार की वर्जनाओं से पूर्णतः मुक्त हैं। ‘पाक साफ़’ और ‘शुद्ध’ कविता की जगह उन्हें ऐसी कविता पसन्द थी जो देह की तरह ही ‘अशुद्ध’ हो। वे धुले-धुलाए, कलफ़ लगाए और लोहा किए वस्त्र जैसी कविता के बदले ऐसी कविता के कायल थे जिनके पहिनने पर खाने-पीने के धब्बे भी हों, जो खेत-खलियान के खर-पात, धूल-धक्कड या फिर कल कारखानों की कालिख-कलौंछ से अलंकृत हों। इसलिए उनकी कविता में रूप के साथ ही उनके लिए भी जगह थी जिसे आम तौर से ‘कुरूप’ कहा जाता है। इस तरह नेरुदा का एक अपना सौन्दर्यशास्त्र था।
वाल्ट ह्विटमैन नेरुदा के अत्यन्त प्रिय कवि थे, बीसवीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका की कारगुजारियों से ख़फ़ा होने के बावजूद। कुछ लोग तो स्वयं पाब्लो नेरुदा को ही दक्षिणी अमेरिका का वाल्ट ह्विटमैन कहते हैं- निश्चय ही बीसवीं शताब्दी का ह्विटमैन-जनता के लोकतन्त्र की सबसे बुलन्द आवाज़ !
नेरुदा की कविता-पुस्तक की तरह पुस्तक मात्र नहीं है, इसे भी जो छूता है, उसे एक ज़िन्दा इनसान को छू लेने का अहसास होता है और उसकी रगों में ख़ून की रफ्तार तेज़ हो जाती है।
नेरुदा की कविताओं में ‘पृथ्वी’ का ज़िक्र अक्सर आता है। उनके एक कविता-संग्रह का नाम ही है ‘पृथ्वी का आवास’। एक कविता है। ‘ठहरो, ओ पृथ्वी’ फिर एक और कविता है ‘तुम में पृथ्वी’ शीर्षक से, जिसके अन्त की दो पंक्तियाँ मन को गहराई तक छू लेती हैं-
नेरुदा मेरे भी प्रिय कवि हैं और उनकी कविताओं का हिन्दी अनुवाद करनेवाले डॉ. चन्द्रबली सिंह तो मेरे आदरणीय अग्रज ही हैं, इसलिए यहाँ कुछ कहने की हिमाकत कर रहा हूँ, वरना स्वयं अनुवादक की विस्तृत भूमिका के बाद कुछ भी कहना ग़ैरज़रूरी है। सबसे पहले तो यही है कि इस पुस्तक के प्रकाशन पर व्यक्तित्व रूप से मुझे जो आत्मसंतोष हुआ वह स्वयं अपनी किसी पुस्तक के प्रकाशन के समय भी नहीं हुआ। कारण यह है कि अनुवाद के उस कठिन जीवन-संघर्ष और आत्मसंघर्ष की गहरी पीड़ा को कुछ-कुछ निकट से देखने का मुझे अवसर मिला है। कोई भी दूसरा व्यक्ति उस संघर्ष में टूटकर बिखर सकता था। शायद यह अनुवाद कर्म की संजीवनी ही है जिसने उन्हें बचाए रखा और आज वे अपनी आँखों अपनी अनवरत साधना को फलीभूत देखने की स्थिति में हैं। वे पक्के परिपूर्णतावादी हैं इतने कि अन्तिम प्रूफ़ की अवस्था तक काट-छाँट, सुधार-सँवार की ज़िद पर अड़े रहे। मुकम्मल पांडुलिपि भी ‘किस तरह खैंच के लाया हूँ कि जी जानता है।’ कहना न होगा कि कविता-वह भी नेरुदा की कविता का अनुवाद चन्द्रबली सिंह के लिए कोई धन्धा नहीं बल्कि गहरी प्रतिबद्धता है।
‘शब्द ख़ून में पैदा होता है’ जैसा कि नेरुदा ने किसी कविता में कहा है और ‘शब्द ही ख़ून को ख़ून और ज़िन्दगी को ज़िन्दगी देते हैं। चन्द्रबली सिंह के इस भाषान्तर के बारे में भी यह बात उतनी ही सच है। उनके अनुवाद की रगों में भी ख़ून बहता दिखाई देता है जिसमें नेरूदा के ख़ून की गरमाहट है।
कुल मिलाकर, कविताओं का अनुवाद कैसा बन पड़ा है, यह तो वही बता सकते हैं जिन्होंने इस मैदान में हाथ आज़माए हैं। एक सामान्य पाठक के नाते सरसरी तौर पर फ़िलहाल मुझे यही लगता है कि स्पेनिश मूल से किए हुए अनुवादों से ये अनुवाद कई जगह हैं और अक्सर अंग्रेज़ी अनुवादों से टक्कर लेते हैं। यह ज़रूर है कि भाषा उतनी चलती हुई नहीं है बल्कि कुछ-कुछ किताबी-सी हो गई है। एक ‘माच्चु पिच्चु के शिखर’ कविता के विभिन्न हिन्दी अनुवादों की तुलना से यह स्पष्ट हो सकती है।
वैसे, ‘माच्चु पिच्चु के शिखर’ नेरुदा की कविता का शिखर भले ही हो, समूचा काव्य संसार नहीं है। इस शिखर के सम्मुख नतमस्तक मैं भी हूँ लेकिन नीचे की घाटियों में ऐसी अनेक जगह हैं। जो कहीं अधिक रम्य और मनोज्ञ हैं। यह विविधता और बहुलता ही नेरुदा की नेरुदा की कविता की प्रकृति है। नेरुदा इतने स्वरों और शैलियों में बोलते हैं कि उनकी कविता को किसी एक साँचे में कसना मुश्किल है। इस तरह ‘नेरुदावाद’ के पहले दुश्मन तो नेरुदा स्वयं हैं।
नेरुदा ने अपनी पचास वर्षों से भी अधिक लम्बी काव्य-यात्रा में कविता को इतनी बार बदला है कि कुछ लोग उन्हें ‘कविता का पिकासो’ कहते हैं।
उनमें किसी भी चीज़ या विषय पर कविता लिखने की असाधारण क्षमता थी। उनके लिए जिसका भी वजूद हो ऐसी हर चीज़ समान रूप से सम्मान के योग्य है और इस नाते वह कविता का विषय भी हो सकती है। कोई चाहे तो इसे कविता का विलक्षण ‘लोकतंत्र’ भी कह सकता है।
इसलिए नेरुदा ऐसी अनपेक्षित जगहों में भी कविता पा जाते थे जहाँ उनकी कोई सम्भावना नहीं होती। सम्भवतः इसी वजह से उनकी प्रत्येक कृति अप्रत्याशित की तरह आती थी। अपनी कविता में वे अक्सर ‘काल्पनिक’ और ‘वास्तविक’ के भेद को इतनी सहजता से मिटा देते हैं कि एक अलौकिक काव्यलोक निर्मित हो जाता है और आगे चलकर गार्सिया मारखेस ने यही काम ‘एकान्तवास के सौ साल’ नामक उपन्यास में किया तो उसे ‘जादुई यथार्थवाद’ का नाम दिया गया। कहना न होगा, इस जादुई यथार्थवाद का प्रयोग नेरुदा पहले ही कर चुके थे और वह भी कविता में। पर 1925 की लिखी उनकी प्रसिद्ध कविता ‘घूमते हुए’ को देखें तो उसमें परस्पर विरोधी और बेमेल बिम्ब इतनी तेज़ रफ़्तार से एक-के-बाद-एक आते हैं कि चकित रह जाना पड़ता है। कविता शुरू होती है इस तरह ‘ऐसा है कि मैं आदमी होने से थक गया हूँ’ और फिर कविता भी घूमते हुए आदमी की तरह ही घूमती रहती है।
सहसा यह पंक्ति आती है ‘जहाँ हड्डियाँ अस्पताल की खिड़कियों के बाहर उड़ती हैं’ और कुछ देर बाद ‘काफी के प्याले में छूट गए नक़ली दाँत’ दिखते हैं। यह एक प्रकार का ‘सुर्रियलज़्म’ यानी ‘अतियथार्थवाद’ है लेकिन जाने-माने ‘अतियथार्थवादियों’ से बिल्कुल अलग। वे अवचेतन के मारे’ सुर्रियलिस्ट’ नहीं, बल्कि अपने आस-पास के चिरपरिचित वातावरण के ‘अतियथार्थवादी’ रूप के ही सहज दर्शक हैं।
नेरुदा की इस तरह की दिलचस्प कविताओं का ज़िक्र इसलिए ज़रूरी है कि उनकी सामान्य छवि केवल एक ‘प्रतिबद्ध’ कम्युनिस्ट कवि की है, जबकि सचाई कुछ और ही है, नेरुदा की पहली कविता-पुस्तक ‘बीस प्रेम कविताएँ और निराशा का एक गीत’ है, जो 1924 में प्रकाशित हुई थी। उस समय नेरुदा बीस की वय के एक युवक थे। इसी कविता-संग्रह ने नेरुदा को सहसा यश के शिखर पर पहुँचा दिया था। कुछ लोग आज उस संग्रह की कविताओं को नेरुदा की सबसे अच्छी कविताओं में गिनते हैं। ‘लिख सकता हूँ सबसे उदास कविताएँ आज की रात’ जैसी लोकप्रिय कविता इसी संग्रह की है। प्रेम कविताओं का यह सिलसिला आगे भी चलता रहा, बल्कि अंतिम वर्षों में तो इस इलाके में बाढ़-सी आ गई। इस्ला नेग्रा (1964) का प्रथम संस्करण तो ‘मातिल्दे उर्रुतिया’ को समर्पित भी है और पूरा संकलन ही जैसे प्रेम पर एक प्रलम्बित अनुचिन्तन है।
नेरुदा प्रेम से भी अधिक काम के कवि हैं। वे उन कवियों में से हैं जो ‘सेक्स’ की वर्जना से सर्वथा मुक्त रहते हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि नेरुदा के लिए काव्य-सर्जना कामभावना का पर्याय जैसा है।
वैसे भी परम स्वच्छन्द नेरुदा सभी प्रकार की वर्जनाओं से पूर्णतः मुक्त हैं। ‘पाक साफ़’ और ‘शुद्ध’ कविता की जगह उन्हें ऐसी कविता पसन्द थी जो देह की तरह ही ‘अशुद्ध’ हो। वे धुले-धुलाए, कलफ़ लगाए और लोहा किए वस्त्र जैसी कविता के बदले ऐसी कविता के कायल थे जिनके पहिनने पर खाने-पीने के धब्बे भी हों, जो खेत-खलियान के खर-पात, धूल-धक्कड या फिर कल कारखानों की कालिख-कलौंछ से अलंकृत हों। इसलिए उनकी कविता में रूप के साथ ही उनके लिए भी जगह थी जिसे आम तौर से ‘कुरूप’ कहा जाता है। इस तरह नेरुदा का एक अपना सौन्दर्यशास्त्र था।
वाल्ट ह्विटमैन नेरुदा के अत्यन्त प्रिय कवि थे, बीसवीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका की कारगुजारियों से ख़फ़ा होने के बावजूद। कुछ लोग तो स्वयं पाब्लो नेरुदा को ही दक्षिणी अमेरिका का वाल्ट ह्विटमैन कहते हैं- निश्चय ही बीसवीं शताब्दी का ह्विटमैन-जनता के लोकतन्त्र की सबसे बुलन्द आवाज़ !
नेरुदा की कविता-पुस्तक की तरह पुस्तक मात्र नहीं है, इसे भी जो छूता है, उसे एक ज़िन्दा इनसान को छू लेने का अहसास होता है और उसकी रगों में ख़ून की रफ्तार तेज़ हो जाती है।
नेरुदा की कविताओं में ‘पृथ्वी’ का ज़िक्र अक्सर आता है। उनके एक कविता-संग्रह का नाम ही है ‘पृथ्वी का आवास’। एक कविता है। ‘ठहरो, ओ पृथ्वी’ फिर एक और कविता है ‘तुम में पृथ्वी’ शीर्षक से, जिसके अन्त की दो पंक्तियाँ मन को गहराई तक छू लेती हैं-
नापती हैं बुमश्किल मेरी आँखें आकाश के और अधिक विस्तार को
और मैं झुकाता हूँ अपने आपको तुम्हारे होठों पर पृथ्वी को चूमने !
और मैं झुकाता हूँ अपने आपको तुम्हारे होठों पर पृथ्वी को चूमने !
नेरुदा के अन्दर ‘पृथ्वी’ का यह गहरा बोध क्या इसलिए था कि वे ऐसी जगह पैदा हुए जो पृथ्वी के दक्षिण भाग का आख़िरी छोर है ? ऐसा लगता है कि नेरुदा उसी आख़िरी छोर पर खड़े होकर पूरी पृथ्वी को अपनी बाँहों में भर लेने की कोशिश करते रहे हैं-निश्चय ही वे बाँहें इतनी विशाल हैं कि उनके घेरे में पृथ्वी भी आ जाती है और प्रिया भी।
नेरुदा का काव्य संसार दक्षिणी चीले के जंगलों, और पहाणों और समुद्र के हरे-भरे वातावरण के साथ-साथ मछुआरों, लकड़हारों तथा दूसरे मेहनतकश लोगों से गुंजान है। इस दृष्टि से नेरुदा ठेठ ‘आंचलिक’ कवि हैं। यह ‘आंचलिकता’ उनकी कविता की जान है। इस प्रसंग में अंतिम काव्यकृतियों में ‘इस्ला नेग्रा’ की कविताएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं क्योंकि वह उनका अन्तिम आवास था। वैसे, ‘इस्ला नेग्रा’ न द्वीप है न ही काला ! पुस्तक भी दरअसल एक तरफ से ‘नोटबुक’ की शक्ल में लिखी हुई कविताओं का संग्रह है, जिसे ‘स्मृतिलेखा भी कहा जा सकता है- गद्य में लिखे हुए ‘मेम्यार’ के बरक्स काव्यात्मक संस्मण अथवा डायरी। इस, संचयन में वह सम्पूर्ण पुस्तक पहली बार हिन्दी में सुलभ हो रही है, जो निश्चय ही एक उपलब्धि है।
यह भी एक विरोधाभाष है कि नेरुदा नितान्त ‘लोकल’ होते हुए भी अपनी विश्व दृष्टि में ‘ग्लोबल’ हैं। उनकी चिन्ता के केन्द्र में निश्चय ही अपने देश के चीले की नियति है, लेकिन वे स्पेन में लोकतन्त्र की रक्षा के लिए लड़ने वालों के साथ भी खड़े थे और फिर मेक्सिको में भी। उनके सम्बन्ध यदि पेरिस और मास्को से थे तो पूरब में रंगून, कोलम्बो और बम्बई से भी उन्हें परिचित होने का अवसर मिला। इस नाते उनकी कविता की बाँहों के घेरे में पश्चिमी गोलार्ध के साथ-साथ पूर्वी गोलार्ध भी सिमटा हुआ है। इस तरह नेरुदा एक विश्वकवि हैं-बीसवीं शताब्दी के विश्वकवियों में सबसे अग्रणी और सम्भवतः भी। इसका एक प्रमाण तो यही है कि जितनी भाषाओं में नेरुदा का अनुवाद हुआ है, उतना अनुवाद इस शताब्दी के किसी और कवि का नहीं हुआ।
विश्वकवि नेरुदा का काव्य-सृजन भी उनके व्यक्तित्व के अनुसार ही विपुल है। लगभग चार हज़ार पृष्ठों की विशाल काव्य सम्पदा वे छोड़ गए हैं और अंग्रेजी में वह पूरी सम्पदा इस वर्ष सुलभ ही करा दी गयी है। फ़िलहाल हिन्दी को प्रस्तुत संचयन से ही संतोष करना पड़ेगा जो समग्र न होते हुए भी हिन्दी में अब तक का सबसे बड़ा चयन है और यथासम्भव नेरुदा का उत्तांश भी। साहित्य अकादमी अपनी गौरवशाली परम्परा के अनुरूप इस संचयन को प्रकाशित करके अपने दायित्व का निर्वाह कर रही है जो सर्वथा उचित है और अभिनन्दनीय भी
शुभमस्तु
नेरुदा का काव्य संसार दक्षिणी चीले के जंगलों, और पहाणों और समुद्र के हरे-भरे वातावरण के साथ-साथ मछुआरों, लकड़हारों तथा दूसरे मेहनतकश लोगों से गुंजान है। इस दृष्टि से नेरुदा ठेठ ‘आंचलिक’ कवि हैं। यह ‘आंचलिकता’ उनकी कविता की जान है। इस प्रसंग में अंतिम काव्यकृतियों में ‘इस्ला नेग्रा’ की कविताएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं क्योंकि वह उनका अन्तिम आवास था। वैसे, ‘इस्ला नेग्रा’ न द्वीप है न ही काला ! पुस्तक भी दरअसल एक तरफ से ‘नोटबुक’ की शक्ल में लिखी हुई कविताओं का संग्रह है, जिसे ‘स्मृतिलेखा भी कहा जा सकता है- गद्य में लिखे हुए ‘मेम्यार’ के बरक्स काव्यात्मक संस्मण अथवा डायरी। इस, संचयन में वह सम्पूर्ण पुस्तक पहली बार हिन्दी में सुलभ हो रही है, जो निश्चय ही एक उपलब्धि है।
यह भी एक विरोधाभाष है कि नेरुदा नितान्त ‘लोकल’ होते हुए भी अपनी विश्व दृष्टि में ‘ग्लोबल’ हैं। उनकी चिन्ता के केन्द्र में निश्चय ही अपने देश के चीले की नियति है, लेकिन वे स्पेन में लोकतन्त्र की रक्षा के लिए लड़ने वालों के साथ भी खड़े थे और फिर मेक्सिको में भी। उनके सम्बन्ध यदि पेरिस और मास्को से थे तो पूरब में रंगून, कोलम्बो और बम्बई से भी उन्हें परिचित होने का अवसर मिला। इस नाते उनकी कविता की बाँहों के घेरे में पश्चिमी गोलार्ध के साथ-साथ पूर्वी गोलार्ध भी सिमटा हुआ है। इस तरह नेरुदा एक विश्वकवि हैं-बीसवीं शताब्दी के विश्वकवियों में सबसे अग्रणी और सम्भवतः भी। इसका एक प्रमाण तो यही है कि जितनी भाषाओं में नेरुदा का अनुवाद हुआ है, उतना अनुवाद इस शताब्दी के किसी और कवि का नहीं हुआ।
विश्वकवि नेरुदा का काव्य-सृजन भी उनके व्यक्तित्व के अनुसार ही विपुल है। लगभग चार हज़ार पृष्ठों की विशाल काव्य सम्पदा वे छोड़ गए हैं और अंग्रेजी में वह पूरी सम्पदा इस वर्ष सुलभ ही करा दी गयी है। फ़िलहाल हिन्दी को प्रस्तुत संचयन से ही संतोष करना पड़ेगा जो समग्र न होते हुए भी हिन्दी में अब तक का सबसे बड़ा चयन है और यथासम्भव नेरुदा का उत्तांश भी। साहित्य अकादमी अपनी गौरवशाली परम्परा के अनुरूप इस संचयन को प्रकाशित करके अपने दायित्व का निर्वाह कर रही है जो सर्वथा उचित है और अभिनन्दनीय भी
शुभमस्तु
!
-नामवर सिंह
भूमिका
पाब्लो नेरुदा की कविताओं का यह संचयन उसके सारे काव्य-संग्रहों में चुनी हुई कविताओं का अनुवाद न होकर उसके दो काव्य-संग्रहों आइला नेग्रा (स्पेनिश में इस्सा नेग्रा) और सर्वशक्तिसम्पन्न की सारी कविताओं का मूल के क्रमानुसार और उसके काव्य-संग्रह कैंटों जेनरल में उसकी लम्बी और सर्वश्रेष्ठ मानी जानेवाली रचना माच्चु पिच्चु के शिखर का अनुवाद है। हिन्दी में नेरुदा की कविताओं के अनुवाद की यह पुस्तक अपने तीन सौ से भी अधिक पृष्ठों के बावजूद उसके कवि-व्यक्तित्व की अन्यतम सम्पन्नता और विविधता का बोध नहीं करा सकती। लेकिन यहाँ तक भी कहने की जरूरत है कि वे इस संचयन की कविताएँ लगभग पाँच दशकों तक अबाध प्रवाहित उसकी सृजनशीलता की महानतम उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
नेरुदा का जन्म 1904 में मध्य चीले के पराल नामक स्थान में हुआ था। उसके बचपन में ही उसे भूकम्प से धवस्त पराल से नये बसाये जा रहे नगर तेमुको में लाया गया, जहाँ उसका पिता रेल विभाग में कर्मचारी था। नेरुदा को अपने बचपन की बहुत ही धुँधली याद थी। लेकिन तेमुको वनों के बीच बसता हुआ एक नया नगर था, जहाँ आवासों से वनों की महक आती थी। यहाँ कवि ने प्रकृति और मानव-जीवन को अभिन्न करके देखना सीखा। उसने आइला नेग्रा की एक कविता, ‘प्रथम यात्रा’ इसका ज़िक्र करते हुए लिखा है-
नेरुदा का जन्म 1904 में मध्य चीले के पराल नामक स्थान में हुआ था। उसके बचपन में ही उसे भूकम्प से धवस्त पराल से नये बसाये जा रहे नगर तेमुको में लाया गया, जहाँ उसका पिता रेल विभाग में कर्मचारी था। नेरुदा को अपने बचपन की बहुत ही धुँधली याद थी। लेकिन तेमुको वनों के बीच बसता हुआ एक नया नगर था, जहाँ आवासों से वनों की महक आती थी। यहाँ कवि ने प्रकृति और मानव-जीवन को अभिन्न करके देखना सीखा। उसने आइला नेग्रा की एक कविता, ‘प्रथम यात्रा’ इसका ज़िक्र करते हुए लिखा है-
मेरे अन्दर वे एक हो जाती थीं,
ज़िन्दगियाँ और पत्तियाँ, (बादामी)
बहार, पुरुष और पेड़।
झंझा और पत्तियों की दुनिया से प्यार करता हूँ।
मेरे लिए होठों और जड़ों में भेद करना संभंव नहीं।
ज़िन्दगियाँ और पत्तियाँ, (बादामी)
बहार, पुरुष और पेड़।
झंझा और पत्तियों की दुनिया से प्यार करता हूँ।
मेरे लिए होठों और जड़ों में भेद करना संभंव नहीं।
किशोरावस्था की इसी स्वप्नमय और लयबद्ध दुनिया को 1920 से 1927 तक सान्तियागो के अध्ययन और युवावस्था के सात वर्षों की शहरी ज़िन्दगी ने ध्वस्त कर दिया। 1924 में प्रणय की बीस कविताएँ और विषाद का एक गान के प्रकाशन के साथ उसे एक असाधारण कविता के कवि के रूप में ख्याति मिली। इसमें प्रणव का यथार्थ ही संदिग्ध है प्रणव अपने पीछे सिर्फ़ यादे, दर्द और अपराध-बोध छोड़ जाता है। संग्रह में ‘आज की रात’ मैं लिख सकता हूँ’ कविता में वह कहता है-
अब मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ, उसमें संदेह नहीं लेकिन शायद उसे प्यार करता हूँ।
प्यार कितना लघुजीवी है, भूलने का समय कितना लम्बा है।
प्यार कितना लघुजीवी है, भूलने का समय कितना लम्बा है।
किशोर नेरुदा को स्कूल में ही नोबेल पुरस्कार विजेता चिलियन शिक्षक और कवि ग्रेब्रियल मिस्ट्रल ने उन्नीसवीं शताब्दी के महान उपन्याकारों से परिचित करवाया था। पुस्तकों की वैविध्यपूर्ण दुनिया की भूख, प्यार की ललक तथा चीले की विषय भूमि और विकट परिस्थितियों में अपने अस्तित्व की रक्षा में जुटे देशवासियों ने उन्हें लिखने के लिए अनगिनत अनुभव आख्यान और विषय दिए। देश के समुद्रतटीय इलाक़ों पर लिखते हुए नेरुदा ने मानवीय भाव और निसर्ग के सौन्दर्य को उन सांसारिक विभीषिकाओं में भी जीवित रखा, जिसने उसके लोगों को कठोर, मजबूत और अन्तर्मुखी बनाया। नेरुदा का उदेश्य था, अपने सभी देशवासियों का रचनात्मक आह्वान जो उन्हें दी गयी दुनिया से जोड़े और जुगाए रखे और साथ ही उन्हें उस उष्मा से परिचित कराए, जो सदियों से उनके अन्दर विद्यमान होते हुए भी ओझल हो गयी थी।
लातिन अमेरिका के बहुत सारे देशों की परम्परा के अनुसार चीले ने असाधारण प्रतिभा के अपने नवोदित कवि को अपना वाणिज्य-दूत बनाकर दक्षिण पूर्व एशिया में भेजा, यहाँ वह 1927 से 1932 तक रंगून, कोलम्बो, सिंगापुर और जावा में कार्यरत रहा। सान्तियागो से भी बढ़कर त्रासद अनुभव उसे इन वर्षों के दौरान हुआ। वह जहाँ भी गया, वहाँ अपने को अजनबी पाया। आइला नेग्रा में उसने कोलम्बो पहुँचने पर कैसा अनुभव किया, इसका उल्लेख ‘वह रोशनी’ कविता में करता है-
लातिन अमेरिका के बहुत सारे देशों की परम्परा के अनुसार चीले ने असाधारण प्रतिभा के अपने नवोदित कवि को अपना वाणिज्य-दूत बनाकर दक्षिण पूर्व एशिया में भेजा, यहाँ वह 1927 से 1932 तक रंगून, कोलम्बो, सिंगापुर और जावा में कार्यरत रहा। सान्तियागो से भी बढ़कर त्रासद अनुभव उसे इन वर्षों के दौरान हुआ। वह जहाँ भी गया, वहाँ अपने को अजनबी पाया। आइला नेग्रा में उसने कोलम्बो पहुँचने पर कैसा अनुभव किया, इसका उल्लेख ‘वह रोशनी’ कविता में करता है-
प्यूमाओं से भी ज़्यादा बेपहचान मैं पहुँचा,
और अपने को अलग रखा, क्योंकि कोई नहीं परिचित था,
शायद इसलिए कि स्वयं उस नशीली रोशनी ने
मेरा दिमाग़ थकाकर चूर-चूर कर दिया था।
और अपने को अलग रखा, क्योंकि कोई नहीं परिचित था,
शायद इसलिए कि स्वयं उस नशीली रोशनी ने
मेरा दिमाग़ थकाकर चूर-चूर कर दिया था।
इस घुटनभरी, अराजक और विघटन होती हुई दुनिया में अपने को अकेला पाकर भी सिर्फ़ ज़िन्दा रहना उसकी क्रूर नियति थी।
यही अनुभव उसके प्रसिद्ध काव्य-संग्रह पृथ्वी पर आवास। (1925-31) और ।। (1931-35) की पृष्ठभूमि है। पृथ्वी पर आवास ।। की एक कविता ‘सिर्फ़ मृत्यु’ इन पक्तियों से शुरू होती है-
यही अनुभव उसके प्रसिद्ध काव्य-संग्रह पृथ्वी पर आवास। (1925-31) और ।। (1931-35) की पृष्ठभूमि है। पृथ्वी पर आवास ।। की एक कविता ‘सिर्फ़ मृत्यु’ इन पक्तियों से शुरू होती है-
एकान्त क़ब्रगाहे होती हैं,
नीरव अस्थियों से पूर्ण समाधियाँ,
हृदय, सुरंग से गुज़रता हुआ
स्याह, स्याह, स्याहः
पोत के ध्वंस की तरह हम अन्तर तक मृत होते हैं,
जैसे हम हृदय के निकट में डूबते या
त्वचा से लेकर आत्मा तक ढह जाते हों
नीरव अस्थियों से पूर्ण समाधियाँ,
हृदय, सुरंग से गुज़रता हुआ
स्याह, स्याह, स्याहः
पोत के ध्वंस की तरह हम अन्तर तक मृत होते हैं,
जैसे हम हृदय के निकट में डूबते या
त्वचा से लेकर आत्मा तक ढह जाते हों
यह अहसास पृथ्वी पर आवास ।। में काफी दूर तक नेरुदा का पीछा करता है। लेकिन उसकी कुछ अन्तिम कविताओं में नेरुदा सोच और शिल्प की एक नयी ज़मीन पर पहुँचने का संकेत देता है। पृथ्वी पर आवास ।।। (1935-45) में वह ज़मीन पूरी उद्घाटित हो जाती है, विशेषतः उन कविताओं में, जिन्हें नेरुदा ने 1937 में स्पेन हमारे दिलों में नाम से एक अलग संकलन के रूप में प्रकाशित किया।
इस संकलन के पीछे वह दाहक अनुभव था, जो नेरुदा ने 1934-36 के दौरान स्पेन में चीले के वाणिज्य-दूत के पद पर काम करते हुए प्राप्त किया था, स्पेन में उसने फ़ासीवाद के उदय, विकास और जनविरोधी हिंस्र और बर्बर चरित्र का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। फ़ासीवादियों ने 1936 में उसके अभिन्न मित्र विश्व-प्रसिद्ध कवि लोर्का की हत्या कर दी। नेरुदा ने फ़ासीवादियों का खुला विरोध किया था। उसे चीले वापस जाना पड़ा। इन अनुभवों ने उसके जीवन, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टिकोण और कविता की सामाजिक भूमिका की समझ को कैसे बदल दिया, इसका उल्लेख उसने पृथ्वी पर आवास ।।। की कविताओं में, आइला नेग्रा की कविता में और अपने मेमोरीज़ (संस्मरण) में किया है। स्पेन हमारे दिलों में की पहली कविता ‘आह्वान’ है और उसके साथ एक संकल्प भी है-
इस संकलन के पीछे वह दाहक अनुभव था, जो नेरुदा ने 1934-36 के दौरान स्पेन में चीले के वाणिज्य-दूत के पद पर काम करते हुए प्राप्त किया था, स्पेन में उसने फ़ासीवाद के उदय, विकास और जनविरोधी हिंस्र और बर्बर चरित्र का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। फ़ासीवादियों ने 1936 में उसके अभिन्न मित्र विश्व-प्रसिद्ध कवि लोर्का की हत्या कर दी। नेरुदा ने फ़ासीवादियों का खुला विरोध किया था। उसे चीले वापस जाना पड़ा। इन अनुभवों ने उसके जीवन, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टिकोण और कविता की सामाजिक भूमिका की समझ को कैसे बदल दिया, इसका उल्लेख उसने पृथ्वी पर आवास ।।। की कविताओं में, आइला नेग्रा की कविता में और अपने मेमोरीज़ (संस्मरण) में किया है। स्पेन हमारे दिलों में की पहली कविता ‘आह्वान’ है और उसके साथ एक संकल्प भी है-
संकल्प एक ऐसे गीत का
जिसमें विस्फोट हों, एक कामना
ऐसे विराट गीत की, ऐसी धातु की
जो युद्ध और नग्न रक्त को समेट सके।
जिसमें विस्फोट हों, एक कामना
ऐसे विराट गीत की, ऐसी धातु की
जो युद्ध और नग्न रक्त को समेट सके।
आइला नेग्रा की कविता, ‘शायद मैं तब से बदल गया हूँ’ में नेरुदा कहता है-
मैं अपने देश अपनी आँखों के नीचे
दूसरी आँखें लेकर पहुँचा
जिन्हें युद्ध ने उस पर आरोपित किया था।
दूसरी आँखें अलाव में
भस्म हो चुकी थीं
जिन्हें स्वयं मेरे आँसुओं ने और अन्यों के रक्त ने
भिंगो डाला था।
और मैंने मानव-संबंधों की कष्टप्रद गहराइयों में
पहले से नीचे जाकर
देखना और झाँकना शुरू किया।
दूसरी आँखें लेकर पहुँचा
जिन्हें युद्ध ने उस पर आरोपित किया था।
दूसरी आँखें अलाव में
भस्म हो चुकी थीं
जिन्हें स्वयं मेरे आँसुओं ने और अन्यों के रक्त ने
भिंगो डाला था।
और मैंने मानव-संबंधों की कष्टप्रद गहराइयों में
पहले से नीचे जाकर
देखना और झाँकना शुरू किया।
उसने अपनी आत्म-कथा मेमोरीज़ (संस्मरण) में भी इसका उल्लेख किया है-‘‘जब पहली गोलियों ने स्पेन के गिटारों को भग्न कर दिया, जब उनसे संगीत की जगह रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी, मेरी कविता आदमी की पीड़ा की राहों में एक प्रेत की तरह निष्प्राण स्थागित हो गई और उसके भीतर से जुड़े और रक्त उमड़ पड़े। तब से मेरा रास्ता आम आदमी के रास्ते से एक हो जाता है और अचानक मैं (चीले के) दक्षिण के एकान्त से उत्तर की तरफ चला आया हूँ, जो सचमुच जनता है, मेरी कविता जिसकी तलवार, जिसका रुमाल होना चाहती है, जिसके विराट दुःखों का स्वेद पोंछ देना चाहती है और जिसे उसके रोटी के संघर्ष में एक अस्त्र देना चाहती है।’’ (पृ. 149)
कविता को आम आदमी तक पहुँचने के लिए नेरुदा अपनी कविताएँ मज़दूरों और राजनीतिक जनसभाओं के बीच सुनने लगा। यह उसका एक नया अनुभव था, जिसने उसके शिल्प पर गहरा प्रभाव डाला। एकाकीपन में स्वगत की भाषा और व्यक्तिनिष्ठ, दुर्बोध बिम्बों की जगह अब सम्बोधन की भाषा और सहज, बोधागम्य बिम्बों ने ले ली। इस संचयन में माच्यु पिच्चु के शिखर (1945), आइला नेग्रा (1962-63) और सर्वशक्तिसम्पन्न (1963) की रचना नेरुदा में इसी क्रान्तिकारी परिवर्तन के बाद हुई।
1938 में नेरुदा ने चीले की जनता के जीवन पर एक महाकाव्यात्मक रचना की योजना के अन्तर्गत लिखना शुरू किया और योजना 1950 में कैंटो जेनरल के प्रकाशन के साथ पूरी हुई। वास्तव में कैंटों जेनरल न सिर्फ़ चीले, बल्कि पूरे लातिन अमरीका की जनता की त्रासद ज़िन्दगी और उसके संघर्षों और स्वप्नों की महागाथा है। इस दौरान पाब्लो नेरुदा की राजनीतिक प्रतिबद्धताएँ दृढ़तर होती गईं। 1945 में वह चीले की संसद का सदस्य चुना गया और उसी वर्ष उसने कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली।
इसी वर्ष पाब्लो नेरुदा ने माच्चु पिच्चु के शिखर की रचना की। स्पेन से लौटने के बाद उसे 1940 में मेक्सिको में चीले के वाणिज्य-दूत के पद पर नियुक्ति मिली। वहाँ तीन वर्ष काम करने के बाद वह अपने देश लौटा। रास्ते में वह जहाँ-जहाँ गया, वहाँ-वहाँ लातिन अमेरिका के एक महान कवि के रूप में उसका भव्य स्वागत किया गया। इसी यात्रा में नेरुदा 1943 में, पेरू में आन्दीज़ में पर्वतमाला में स्थिति माच्चु पिच्चु देखने के लिए गया। इसके दो वर्ष बाद, 1945 में, उसने माच्चु पिच्चु के शिखर की रचना की।
कविता को आम आदमी तक पहुँचने के लिए नेरुदा अपनी कविताएँ मज़दूरों और राजनीतिक जनसभाओं के बीच सुनने लगा। यह उसका एक नया अनुभव था, जिसने उसके शिल्प पर गहरा प्रभाव डाला। एकाकीपन में स्वगत की भाषा और व्यक्तिनिष्ठ, दुर्बोध बिम्बों की जगह अब सम्बोधन की भाषा और सहज, बोधागम्य बिम्बों ने ले ली। इस संचयन में माच्यु पिच्चु के शिखर (1945), आइला नेग्रा (1962-63) और सर्वशक्तिसम्पन्न (1963) की रचना नेरुदा में इसी क्रान्तिकारी परिवर्तन के बाद हुई।
1938 में नेरुदा ने चीले की जनता के जीवन पर एक महाकाव्यात्मक रचना की योजना के अन्तर्गत लिखना शुरू किया और योजना 1950 में कैंटो जेनरल के प्रकाशन के साथ पूरी हुई। वास्तव में कैंटों जेनरल न सिर्फ़ चीले, बल्कि पूरे लातिन अमरीका की जनता की त्रासद ज़िन्दगी और उसके संघर्षों और स्वप्नों की महागाथा है। इस दौरान पाब्लो नेरुदा की राजनीतिक प्रतिबद्धताएँ दृढ़तर होती गईं। 1945 में वह चीले की संसद का सदस्य चुना गया और उसी वर्ष उसने कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली।
इसी वर्ष पाब्लो नेरुदा ने माच्चु पिच्चु के शिखर की रचना की। स्पेन से लौटने के बाद उसे 1940 में मेक्सिको में चीले के वाणिज्य-दूत के पद पर नियुक्ति मिली। वहाँ तीन वर्ष काम करने के बाद वह अपने देश लौटा। रास्ते में वह जहाँ-जहाँ गया, वहाँ-वहाँ लातिन अमेरिका के एक महान कवि के रूप में उसका भव्य स्वागत किया गया। इसी यात्रा में नेरुदा 1943 में, पेरू में आन्दीज़ में पर्वतमाला में स्थिति माच्चु पिच्चु देखने के लिए गया। इसके दो वर्ष बाद, 1945 में, उसने माच्चु पिच्चु के शिखर की रचना की।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book