|
बहुभागीय पुस्तकें >> यशपाल की सम्पूर्ण कहानियाँ - भाग 1 यशपाल की सम्पूर्ण कहानियाँ - भाग 1यशपाल
|
70 पाठक हैं |
||||||
यशपाल की सम्पूर्ण कहानियों का पहला भाग...
इस पुस्तक का सेट खरीदें।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्रथम भाग में ‘पिजड़े की उड़ान’ ‘वो
दुनिया’ ’ज्ञानदान‘ और ‘अभिशप्त’ कथा-संकलनों की कहानियाँ
संग्रहित हैं। 1938 में प्रकाशित अपनी प्रथम कहानी संकलन ‘पिजड़े की
उड़ान’ में यशपाल पहली और अन्तिम बार कथा सृजन में कल्पना की
भूमिका को स्वीकार करते हैं। यद्यपि इसका विस्तार कथा-वस्तु के चयन और
कहानी के रूप में विन्यास के बाद में भी जितना और जैसा उन्होंने किया है,
वैसा हिन्दी के कलावादी लेखक भी नहीं कर पाये हैं। लेकिन उन्हें हमेशा लगा
जैसे कल्पना की महती भूमिका को स्वीकार कर लेने पर साहित्य को यथार्थवादी
दृष्टि पर आँच आ सकती है।
‘पिजड़े की उड़ान’ की अधिकांश कहानियाँ जेल में लिखी गयी थीं। वे बाह्य संसार से अलग काल कोठरी में बन्द थे इसलिए उनके पास मात्र कल्पना का ही अवलम्ब था जिसके माध्यम से वे बाह्य संसार को देख और महसूस कर सकते थे। कहना न होगा कि जेल में लिखी गयी इन कहानियों ने हिन्दी संसार को चमत्कृत कर दिया। ‘मक्रील’ जैसी कोमल, संवेदनात्मक कहानी दुबारा यशपाल-साहित्य में दिखाई नहीं पड़ी।
जेल में छूटने के बाद वे जीवन की कठोर भूमि पर उतर आये वस्तुगत यथार्थ की काँटों भरी राह पर जल पड़े। फिर तो ‘वो दुनियाँ’ से आगे बढ़कर ‘ज्ञानदान’ तक आते लोगों की आँखें खोलने के लिए वे सच्चाइयों के चेहरे नकाब उठाने लगे। गहरी नींद में डूबे समाज को जगाने का उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सुझता था इसलिए उन्होंने अपनी कहानियों को ही वह उपादान बना दिया और ‘अभिशप्त’ की कहानियों तक पहुँचते-पहुँचते कहानी साहित्य को सर्वथा नये शिल्प, नये कथा बोध को ऐसा रूप दे दिया जैसे हिन्दी साहित्य में अब तक कुछ अन्य नहीं था। कलावादियों और प्रगतिशीलों से अलग यशपाल और उनकी कहानियों की धमनी एक निजी पहचान बन गयी।
हिन्दी कहानी की विकास परम्परा में यशपाल अकेले लेखक हैं, जिसमें यथार्थवादी रचनादृष्टि के अनेक स्तर और अनेक रूप विद्यमान है कथा-वस्तु ही नहीं, शिल्प के स्तर पर भी उनका अवदान हिन्दी कहानी में ऐसा है जिसे रेखांकित किया जाना बाकी है। परम्परागत कथा-रूप से लेकर आख्यान के शिल्प तक इनके प्रयोगों का विस्तार है। कथा-वस्तु के क्षेत्र में कल्पना से लेकर यथार्थ और फिर सामाजिक यथार्थ की सहज भूमिका पर उतर कर अन्वेषण और उद्घाटन तक उनका कथा-सृजन फैला हुआ है। इस तरह देखो तो वे हिन्दी कहानी के एक मात्र ऐसे स्त्रष्टा हैं जिन्होंने कल्पना प्रसूत, भावात्मक सृजन से शुरू करके कथा वाचन तक को लम्बी कथा यात्रा इन कहानियों में पूरी की है। आख्यायिका के शिल्प तक पहुँचते-पहुँचते यशपाल कहानी को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानने लगते हैं।
1939 से 1979 के बीच प्रकाशित सत्रह कथा-संकलनों में फैला हुआ उनका विशाल कहानी लेखन हिन्दी साहित्य की गौरवपूर्ण उपलब्धि है जिसे अब ’लोकभारती‘ चार भागों में प्रकाशित कर ऐसे पाठक वर्ग तथा पुस्तकालयों की माँग को पूरा कर रहा हैं जो एक लम्बे अरसे से यशपाल की कहानियों के ग्रन्थावली-रूप की माँग कर रहा था।
इसके प्रकाशन में इसका ध्यान रखा गया है कि लेखक के रचनात्मक विकास की पूरी प्रक्रिया अक्षुण्ण बनी रहे। अनुक्रम से संकलन का नाम और उनमें प्रकाशित कहानियों का पर्ववर्ती क्रम जैसा का तैसा रखा गया है।
‘पिजड़े की उड़ान’ की अधिकांश कहानियाँ जेल में लिखी गयी थीं। वे बाह्य संसार से अलग काल कोठरी में बन्द थे इसलिए उनके पास मात्र कल्पना का ही अवलम्ब था जिसके माध्यम से वे बाह्य संसार को देख और महसूस कर सकते थे। कहना न होगा कि जेल में लिखी गयी इन कहानियों ने हिन्दी संसार को चमत्कृत कर दिया। ‘मक्रील’ जैसी कोमल, संवेदनात्मक कहानी दुबारा यशपाल-साहित्य में दिखाई नहीं पड़ी।
जेल में छूटने के बाद वे जीवन की कठोर भूमि पर उतर आये वस्तुगत यथार्थ की काँटों भरी राह पर जल पड़े। फिर तो ‘वो दुनियाँ’ से आगे बढ़कर ‘ज्ञानदान’ तक आते लोगों की आँखें खोलने के लिए वे सच्चाइयों के चेहरे नकाब उठाने लगे। गहरी नींद में डूबे समाज को जगाने का उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सुझता था इसलिए उन्होंने अपनी कहानियों को ही वह उपादान बना दिया और ‘अभिशप्त’ की कहानियों तक पहुँचते-पहुँचते कहानी साहित्य को सर्वथा नये शिल्प, नये कथा बोध को ऐसा रूप दे दिया जैसे हिन्दी साहित्य में अब तक कुछ अन्य नहीं था। कलावादियों और प्रगतिशीलों से अलग यशपाल और उनकी कहानियों की धमनी एक निजी पहचान बन गयी।
हिन्दी कहानी की विकास परम्परा में यशपाल अकेले लेखक हैं, जिसमें यथार्थवादी रचनादृष्टि के अनेक स्तर और अनेक रूप विद्यमान है कथा-वस्तु ही नहीं, शिल्प के स्तर पर भी उनका अवदान हिन्दी कहानी में ऐसा है जिसे रेखांकित किया जाना बाकी है। परम्परागत कथा-रूप से लेकर आख्यान के शिल्प तक इनके प्रयोगों का विस्तार है। कथा-वस्तु के क्षेत्र में कल्पना से लेकर यथार्थ और फिर सामाजिक यथार्थ की सहज भूमिका पर उतर कर अन्वेषण और उद्घाटन तक उनका कथा-सृजन फैला हुआ है। इस तरह देखो तो वे हिन्दी कहानी के एक मात्र ऐसे स्त्रष्टा हैं जिन्होंने कल्पना प्रसूत, भावात्मक सृजन से शुरू करके कथा वाचन तक को लम्बी कथा यात्रा इन कहानियों में पूरी की है। आख्यायिका के शिल्प तक पहुँचते-पहुँचते यशपाल कहानी को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानने लगते हैं।
1939 से 1979 के बीच प्रकाशित सत्रह कथा-संकलनों में फैला हुआ उनका विशाल कहानी लेखन हिन्दी साहित्य की गौरवपूर्ण उपलब्धि है जिसे अब ’लोकभारती‘ चार भागों में प्रकाशित कर ऐसे पाठक वर्ग तथा पुस्तकालयों की माँग को पूरा कर रहा हैं जो एक लम्बे अरसे से यशपाल की कहानियों के ग्रन्थावली-रूप की माँग कर रहा था।
इसके प्रकाशन में इसका ध्यान रखा गया है कि लेखक के रचनात्मक विकास की पूरी प्रक्रिया अक्षुण्ण बनी रहे। अनुक्रम से संकलन का नाम और उनमें प्रकाशित कहानियों का पर्ववर्ती क्रम जैसा का तैसा रखा गया है।
प्रकाशकीय
हिन्दी कहानी की विकास परम्परा में वस्तु और शिल्प दोनों दृष्टियों से
यशपाल की कहानियों के वैशिष्ट्य के लिए आज भी कोई चुनौती नहीं है। वे अपनी
तरह के अकेले सर्जक हैं जिनका समस्त साहित्य जनता के लिए समर्पित है। उनकी
मान्यता भी यही थी कि सामाजिक विकास की निस्तरता से उत्पन्न वास्तविकताओं
को अनावृत्त और विश्लेषित करते रहने की श्रेष्ठतर दूसरा मन्तव्य साहित्य
का नहीं हो सकता। 1939 में उनका पहला कहानी संग्रह ‘पिंजड़े की
उड़ान’ प्रकाश में आया तब यशपाल जीवनानुभवों के मार्ग का एक पूरा
घटना बहुल सफर तय कर चुके थे। वैचारिक प्रयोगों की सफलता-असफलता से जूझते
हुए, वहाँ पहुँच चुके थे जिसके आगे शायद मार्ग अवरुद्ध था। 1919 के रौलेट
एक्ट का प्रभाव उन पर पहला माना गया है।
तब तक वे अपनी पारिवारिक आर्य समाजी परम्परा के साथ जुड़े हुए थे और ट्यूशन करके परिवार की आर्थिक स्थित में अपना अंशदान देने लगे थे। फिरोजपुर छावनी में उस समय जो भी काँग्रेसी आन्दोलन चला उसमें यशपाल की सक्रिय भूमिका का उल्लेख किया जाता है। इतना ही नहीं 1921 में चौरा-चौरी काण्ड के बाद गाँधी जी द्वारा आन्दोलन की वापसी से देश के अनेक नौजवानों की तरह यशपाल को भी भारी निराशा हुई। वे सरकारी कालेज में पढ़ना नहीं चाहते थे। इसी कारण लाला लाजपत राय के नेशनल कालेज में भर्ती हो गए। यहीं उनका परिचय भगत सिंह, सुखदेव और भगवतीचरण से हुआ। जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिए गाँधीवाद मार्ग से अलग क्रान्तिकारी रास्ते पर चलकर स्वतन्त्रता के निमित्त अपना जीवन अर्पित करने का निश्चय लिया था। वे लोग तो कुछ ही दिन बाद भूमिगत हो गए लेकिन यशपाल नेशनल कालेज में पढ़ाते हुए दल का सूत्र संभालने लगे।
भगत सिंह और यशपाल दोनों की साहित्य में गहरी दिलचस्पी थी। उदयशंकर भट्ट उसी कालेज में अध्यापक थे। और उन्हीं की प्रेरणा से यशपाल ने पहली कहानी हिन्दी के मासिक पत्र में प्रकाशित हुई। कानपुर के ‘प्रताप’ ने भी उनकी कुछ भावात्मक गद्य की तरह की रचनाएँ छापीं लेकिन इसे यशपाल के लेखकीय जीवन की शुरुआत मानना भूल होगी। वे तो दिन पर दिन क्रान्तिकारी आन्दोलन की भारी जिम्मेदारियों में व्यस्त होते जा रहे थे। जहाँ कुछ निश्चय थे और उनसे निसृत कार्यक्रमों का व्यस्तता भरा दौर था।
1928 में लाला लाजपत राय पर आक्रमण करने वाले सार्जेण्ट साण्डर्स को गोली मारी गयी। 1929 मार्च में भगत सिंह ने दिल्ली असेम्बली में बम फेंका। 1929 में लाहौर में एक बम फैक्ट्री पकड़ी गई। तनाव इतना बढ़ा कि यशपाल भूमिगत हो गये। कहते हैं 1929 में ही वायसराय की गाड़ी के नीचे क्रान्तिकारियों ने जो बम विस्फोट किया वह यशपाल के हाथों हुआ था।
जाहिर है कि यशपाल को लम्बे समय का भूमिगत जीवन बिताते हुए ‘‘हिन्दुस्तानी समाजवादी प्रजातन्त्र सेना’’ का काम सम्भालना पड़ा। 1931 में इस सेना के कमाण्डर इन चीफ चन्द्रशेखर आजाद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में गोली मार दी गयी। यशपाल सेना के कमाण्डर इन चीफ बनाये गये इसी समय लाहौर षड्यन्त्र का मुकदमा चल रहा था। यशपाल उनके प्रधान अभियुक्त थे। 1932 में यशपाल और दूसरे क्रान्तिकारी भी गिरफ्तार हो गये। उन्हें चौदह वर्ष का सख्त कारावास हुआ। 1938 में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल आने पर राजनैतिक कैदियों की रिहाई हुई और यशपाल 2 मार्च 1938 को जेल से छूट गये। उन्हें लाहौर जाने की मनाही थी इसलिए लखनऊ को उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया। विप्लव का प्रकाश और उनके साहित्यिक जीवन के शुरुआत का यही काल है।
ध्यान देने की बात है कि ऊपर दिया गया है एक विहंगम विवरण यशपाल के महान समरगाथा जैसे जीवन का मात्र एक ट्रेलर है। जिसके अन्यत्र अन्तर मार्गों में न जाने कितना कुछ ऐसा होगा, जिसमें भावात्मक और संवेदनात्मक तनावों के साथ वास्तविक अनुभवों के एक विराट संसार छिपा होगा—चरित्रों और घटनाओं की विपुलता के साथ मानवीय प्रकृति के बारीक अनुभवों के उल्टे-सीधे तन्तुओं का महाजाल फैला होगा जो उनके विशाल कहानी साहित्य में फैला हुआ है।
हमारे लिए उनके कथा-संकलनों को कुछ एक भागों में संकलित करते हुए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा अन्ततः निश्चय यह हुआ कि 1939 से 1979 के बीच प्रकाशित उनके 18 कथा संकलनों को काल-क्रमानुसार चार भागों में बाँट कर प्रकाशित किया जाय। कथा साहित्य के मर्मज्ञ आलोचकों और विद्वानों ने भी इसी को उचित बताया। इससे उनके रचनात्मक विकास का एक सम्पूर्ण चित्र हिन्दी पाठकों को प्राप्त हो सकेगा। इन संकलनों के बारे में आपके सुझाव और सम्मति की हमें सदा प्रतीक्षा रहेगी।
तब तक वे अपनी पारिवारिक आर्य समाजी परम्परा के साथ जुड़े हुए थे और ट्यूशन करके परिवार की आर्थिक स्थित में अपना अंशदान देने लगे थे। फिरोजपुर छावनी में उस समय जो भी काँग्रेसी आन्दोलन चला उसमें यशपाल की सक्रिय भूमिका का उल्लेख किया जाता है। इतना ही नहीं 1921 में चौरा-चौरी काण्ड के बाद गाँधी जी द्वारा आन्दोलन की वापसी से देश के अनेक नौजवानों की तरह यशपाल को भी भारी निराशा हुई। वे सरकारी कालेज में पढ़ना नहीं चाहते थे। इसी कारण लाला लाजपत राय के नेशनल कालेज में भर्ती हो गए। यहीं उनका परिचय भगत सिंह, सुखदेव और भगवतीचरण से हुआ। जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिए गाँधीवाद मार्ग से अलग क्रान्तिकारी रास्ते पर चलकर स्वतन्त्रता के निमित्त अपना जीवन अर्पित करने का निश्चय लिया था। वे लोग तो कुछ ही दिन बाद भूमिगत हो गए लेकिन यशपाल नेशनल कालेज में पढ़ाते हुए दल का सूत्र संभालने लगे।
भगत सिंह और यशपाल दोनों की साहित्य में गहरी दिलचस्पी थी। उदयशंकर भट्ट उसी कालेज में अध्यापक थे। और उन्हीं की प्रेरणा से यशपाल ने पहली कहानी हिन्दी के मासिक पत्र में प्रकाशित हुई। कानपुर के ‘प्रताप’ ने भी उनकी कुछ भावात्मक गद्य की तरह की रचनाएँ छापीं लेकिन इसे यशपाल के लेखकीय जीवन की शुरुआत मानना भूल होगी। वे तो दिन पर दिन क्रान्तिकारी आन्दोलन की भारी जिम्मेदारियों में व्यस्त होते जा रहे थे। जहाँ कुछ निश्चय थे और उनसे निसृत कार्यक्रमों का व्यस्तता भरा दौर था।
1928 में लाला लाजपत राय पर आक्रमण करने वाले सार्जेण्ट साण्डर्स को गोली मारी गयी। 1929 मार्च में भगत सिंह ने दिल्ली असेम्बली में बम फेंका। 1929 में लाहौर में एक बम फैक्ट्री पकड़ी गई। तनाव इतना बढ़ा कि यशपाल भूमिगत हो गये। कहते हैं 1929 में ही वायसराय की गाड़ी के नीचे क्रान्तिकारियों ने जो बम विस्फोट किया वह यशपाल के हाथों हुआ था।
जाहिर है कि यशपाल को लम्बे समय का भूमिगत जीवन बिताते हुए ‘‘हिन्दुस्तानी समाजवादी प्रजातन्त्र सेना’’ का काम सम्भालना पड़ा। 1931 में इस सेना के कमाण्डर इन चीफ चन्द्रशेखर आजाद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में गोली मार दी गयी। यशपाल सेना के कमाण्डर इन चीफ बनाये गये इसी समय लाहौर षड्यन्त्र का मुकदमा चल रहा था। यशपाल उनके प्रधान अभियुक्त थे। 1932 में यशपाल और दूसरे क्रान्तिकारी भी गिरफ्तार हो गये। उन्हें चौदह वर्ष का सख्त कारावास हुआ। 1938 में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल आने पर राजनैतिक कैदियों की रिहाई हुई और यशपाल 2 मार्च 1938 को जेल से छूट गये। उन्हें लाहौर जाने की मनाही थी इसलिए लखनऊ को उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया। विप्लव का प्रकाश और उनके साहित्यिक जीवन के शुरुआत का यही काल है।
ध्यान देने की बात है कि ऊपर दिया गया है एक विहंगम विवरण यशपाल के महान समरगाथा जैसे जीवन का मात्र एक ट्रेलर है। जिसके अन्यत्र अन्तर मार्गों में न जाने कितना कुछ ऐसा होगा, जिसमें भावात्मक और संवेदनात्मक तनावों के साथ वास्तविक अनुभवों के एक विराट संसार छिपा होगा—चरित्रों और घटनाओं की विपुलता के साथ मानवीय प्रकृति के बारीक अनुभवों के उल्टे-सीधे तन्तुओं का महाजाल फैला होगा जो उनके विशाल कहानी साहित्य में फैला हुआ है।
हमारे लिए उनके कथा-संकलनों को कुछ एक भागों में संकलित करते हुए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा अन्ततः निश्चय यह हुआ कि 1939 से 1979 के बीच प्रकाशित उनके 18 कथा संकलनों को काल-क्रमानुसार चार भागों में बाँट कर प्रकाशित किया जाय। कथा साहित्य के मर्मज्ञ आलोचकों और विद्वानों ने भी इसी को उचित बताया। इससे उनके रचनात्मक विकास का एक सम्पूर्ण चित्र हिन्दी पाठकों को प्राप्त हो सकेगा। इन संकलनों के बारे में आपके सुझाव और सम्मति की हमें सदा प्रतीक्षा रहेगी।
-प्रकाशक
मक्रील
गरमी का मौसम था। ‘मक्रील’ की सुहावनी पहाड़ी। आबोहवा
में
छुट्टी के दिन बिताने के लिए आयी सम्पूर्ण भद्र जनता खिंच कर मोटर के
अड्डे पर—जहाँ पंजाब से आगे वाली सड़क की गाड़ियाँ ठहरती
हैं—एकत्र हो रही थी। सूर्य पश्चिम ओर देवदरों से छायी पहाड़ी
को
चोटी के पीछे सरक गया था। सूर्य का अवशिष्ट प्रकाश चोटी पर उगे देवदारों
से ढँकी आग की दीवार के समान जान पड़ता था।
ऊपर आकाश में मोर-पूँछ के आकार में दूर-दूर तक सिंदूर फैल रहा था। उस गहरे अर्गवानी रंग के पर्दे पर ऊँची, काली चोटियाँ निश्चल, शान्त और गम्भीर खड़ी थी। संध्या के झीने अँधेरे में पहाड़ियों के पार्श्व के वनों से पक्षियों का कलरव तुमुल परिमाण में उठ रहा था। वायु में चीड़ की तीखी गन्ध भर रही थी। सभी ओर उत्साह, अमंग और चलह-पहल थी। भद्र महिलाओं और पुरुषों के समूह राष्ट्र के मुकुट और उज्ज्वल करने वाले कवि के सम्मान के लिए उतावले हो रहे थे।
योरुप और अमेरिका ने जिसकी प्रतिभा का लोहा मान लिया, जो देश के इतने अभिमान की सम्पत्ति है, वही कवि ‘मक्रील’ में कुछ दिन स्वास्थ्य सुधारने के लिए आ रहा है। मक्रील में जमी राष्ट्र-अभिमानी जनता, पलकों के पाँवड़े डाल उसकी अगवानी के लिए आतुर हो रही थी।
पहाड़ियों की छाती पर खिंची धूसर लकीर-सी सड़क पर धूल का एक बादल-सा दिखाई दिया। जनता की उत्सुक नजरें और उँगलियाँ उस ओर उठ गयीं। क्षण भर में धूल के बादल को फाड़ती हुई काले रंग की एक गतिमान वस्तु दिखाई दी। वह मोटर थी। आनन्द की हिलोर से जनता का समूह लहरा उठा। देखते ही देखते मोटर आ पहुँची।
जनता की उन्मत्तता के कारण मोटर को दस कदम पीछे ही रुक जाना पड़ा—‘देश के सिरताज की जय !’ सरस्वती के वरद पुत्र की जय !’ राष्ट्र के मुकुट-मणि की जय !’ के नारों से पहाड़ियाँ गूँज उठीं।
मोटर फूलों से भर गयी। बड़ी चहल-पहल के बाद जनता से घिरा हुआ, गजरों के बोझ से गर्दन झुकाए शनैः-शनैः कदम रखता हुआ मक्रील का अतिथि मोटर के अड्डे से चला।
उत्साह से बावली जनता विजयनाद करती हुई आगे-पीछे चल रही थी। जिन्होंने कवि का चेहरा देख पाया, वे भाग्यशाली विरले ही थे। ‘धवलगिरि’ होटल में दूसरी मंजिल पर कवि को टिकाने की व्यवस्था की गयी थी। वहाँ उसे पहुँचा, बहुत देर तक उसके आराम में व्याघात कर, जनता अपने स्थान को लौट आयी।
क्वार की त्रयोदशी का चन्द्रमा पार्वत्य-प्रदेश के निर्मल आकाश में ऊँचा उठ अपनी शीतल आभा से आकाश और पृथ्वी को स्तंभित किए हुए था। उस दूध की बौछार में ‘धवलिगिरि’ की हिमधवल दोमंज़िली इमारत चाँदी की दीवार-सी चमक रही थी। होटल के आँगन की फुलवारी में खूब चाँदनी थी, परन्तु उत्तर-पूर्व के भाग में इमारत के बाजू की छाया पड़ने से अँधेरा था। बिजली के प्रकाश से चमकती खिड़कियों के शीशों और पर्दों के पीछे से आने वाली मर्मध्वनि तथा नौकरों के चलने-फिरने की आवाज के अतिरिक्त सब शान्त था।
उस समय इस अँधेरे बाजू के नीचे के कमरे में रहने वाली एक युवती, फुलवारी के अन्धकारमय भाग में एक सरो के पेड़ के समीप खड़ी, दूसरी मंजिल में पुष्प-तोरणों से सजी उन खिड़कियों की ओर दृष्टि लगाये थी, जिनमें सम्मानित कवि को ठहराया गया था।
वह युवती भी उस आवेगमय स्वागत में सम्मिलित थी। पुलकित हो उसने ‘कवि’ पर फूल फेंके थे, जयनाद भी किया था। उस घमासान भीड़ में समीप पहुँच एक आँख के कवि देख लेने का अवसर उसे न मिला था। इसी साध को मन में लिये वह उस खिड़की की ओर टकटकी लगाए खड़ी थी। काँच पर कवि के शरीर की छाया उसे जब-तब दिखाई पड़ जाती।
स्फूर्तिप्रद भोजन के पश्चात कवि ने बरामदे में आ काले पहाडों के ऊपर चन्द्रमा के मोहक प्रकाश को देखा। सामने सँकरी धुँधली घाटी में बिजली की लपक की तरह फैली हुई मक्रील की धारा की ओर नजर गयी। नदी के प्रवाह की गम्भीर घरघराहट को सुन वह सिहर उठा। कितने ही क्षण मुँह उठाए वह मुग्ध भाव से खड़ा रहा। मक्रील नदी के उद्दाम प्रवाह के उस उज्ज्वल चाँदनी में देखने की इच्छा से कवि की आत्मा व्याकुल हो उठी। आवेश और उन्मेष का वह पुतला सौंदर्य के इस आह्वान की उपेक्षा न कर सका।
सरो वृक्ष के समीप खड़ी युवती पुलकित भाव से देश-कीर्ति के उस उज्ज्वल नक्षत्र को प्यासी आँखों से देख रही थी। चाँद के धुँधले प्रकाश में उसने इतनी दूर से उसने जो भी देख पाया, उसी से संतोष की साँस ले उसने श्रद्धा से सिर नवा दिया। इसे ही अपना सौभाग्य समझ वह चलने को थी कि लम्बा ओवरकोट पहने, छड़ी हाथ में लिये, दायीं ओर जीने से नीचे आता कवि दिखायी पड़ा। पल भर में कवि फुलवारी में आ पहुँचा।
फुलवारी में पहुँचने पर कवि को स्मरण हुआ, ख्यातनामा मक्रील नदी का मार्ग तो वह जानता ही नहीं। इस अज्ञान की अनुभूति से कवि ने दायें-बायें सहायता की आशा से देखा। समीप खडी़ एक युवती को देख, भद्रता से टोपी छूते हुए उसने पूछा—‘‘आप भी इस होटल में ठहरी हैं ?’’
सम्मान से सिर झुकाकर युवती ने उत्तर दिया—‘‘जी हाँ।’’
झिझकते हुए कवि ने पूछा—‘‘मक्रील नदी समीप ही किस ओर है, शायद आप जानती होंगी ?’’
उत्साह से कदम बढ़ाते हुई युवती बोली—‘‘जी हाँ। यही सौ कदम पर पुल है।’’
और मार्ग दिखाने के लिए वह प्रस्तुत हो गयी।
युवती के खुले मुख पर चन्द्रमा का प्रकाश पड़ रहा था। पतली भावों के नीचे बड़ी-बड़ी आँखों में मक्रील की उज्ज्वलता झलक रही थी।
कवि ने संकोच से कहा—‘‘न, न आपको व्यर्थ कष्ट होगा।’’
गौरव से युवती बोली—‘‘कुछ भी नहीं—यही तो है, सामने !’’
...उजली रात में संगमरमर की सुघड़ सुंदर सजीव मूर्ति-सी युवती...साहसमयी, विश्वासमयी मार्ग दिखाने चली सुन्दरता के याचक कवि को। कवि की कविता वीणा के सूक्ष्म तार स्पन्दित हो उठे...सुन्दरता स्वयं अपना परिचय देने चली...सृष्टि सौंदर्य के सरोवर की लहर उसे दूसरी लहर से मिलाने ले जा रही है—कवि ने सोचा।
सौ कदम पर मक्रील का पुल था। दो पहाड़ियों के तंग दर्रे में से उद्दाम वेग और घनघोर शब्द से बहते हुए जल के ऊपर तारों के रस्सों में झूलता हलका-सा पुल लटक रहा था। वे दोनों पुल के ऊपर जा खड़ा हुए। नीचे तीव्र वेग से लाखों-करोड़ों पिघले हुए चाँद बहते चले जा रहे थे, पार्श्व की चट्टानों से टकरा कर वे फेनिल हो उठते। फेनराशि से दृष्टि न हटा कवि ने कहा—‘‘सौंदर्य उन्मत्त हो उठा है।’’ युवती को जान पड़ा, मानो प्रकृति मुखरित हो उठी है।
कुछ क्षण पश्चात कवि बोला—‘‘आवेग में ही सौंदर्य का चरम विकास है। आवेग निकल जाने पर केवल कीचड़ रह जाता है।
युवती तन्मयता से उन सब्दों को पी रही थी। कवि ने कहा—‘‘अपने जन्म-स्थान पर मक्रील न इतनी वेगवती होगी, न इतनी उद्दा। शिशु की लटपट चाल से वह चलती होगी, समुद्र में पहुँच वह प्रौढ़ता की सिथिल गंभीरता धारण कर लेगी।’’
‘‘और मक्रील ! तेरा समय यही है। फूल न खिल जाने से पहले इतना सुन्दर होता है और न तब जब उसकी पँखुड़ियाँ लटक जायँ। उसका असली समय वही है, जब वह स्पुटोन्मुख हो। मधुमाखी उस समय पर निछावर होने के लिए मतवाली हो उठती है।’’ एक दीर्घ निःश्वास छो़ड़, आँखें झुका, कवि चुप हो गया।
मिनिट पर मिनिट गुजरने लगे। सर्द पहाड़ी हवा के झोंके से कवि के वृद्ध शरीर को समय का ध्यान आया। उसने देखा, मक्रील की फेनिल श्वेत, युवती की सुघड़ता पर विराज रही है। एक क्षण के लिए कवि, ‘‘घोर शब्दमयी प्रवाहमयी’ युवती को भूल मूक युवती का सौंदर्य निहारने लगा। हवा के दूसरे झोंके से सिहर कर वह बोला—‘‘समय अधिक हो गया है, चलना चाहिए।’’
लौटते समय मार्ग में कवि ने कहा—‘‘ आज त्रयोदशी के दिन यह शोभा है। कल और भी अधिक प्रकाश होगा। यदि असुविधा न हो तो क्या कल भी मारग दिखाने आओगी ?’’ और स्वयं ही संकोच के चाबुक की चोंट कर वह हँस पड़ा।
युवती ने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया—‘‘अवश्य।’’
ऊपर आकाश में मोर-पूँछ के आकार में दूर-दूर तक सिंदूर फैल रहा था। उस गहरे अर्गवानी रंग के पर्दे पर ऊँची, काली चोटियाँ निश्चल, शान्त और गम्भीर खड़ी थी। संध्या के झीने अँधेरे में पहाड़ियों के पार्श्व के वनों से पक्षियों का कलरव तुमुल परिमाण में उठ रहा था। वायु में चीड़ की तीखी गन्ध भर रही थी। सभी ओर उत्साह, अमंग और चलह-पहल थी। भद्र महिलाओं और पुरुषों के समूह राष्ट्र के मुकुट और उज्ज्वल करने वाले कवि के सम्मान के लिए उतावले हो रहे थे।
योरुप और अमेरिका ने जिसकी प्रतिभा का लोहा मान लिया, जो देश के इतने अभिमान की सम्पत्ति है, वही कवि ‘मक्रील’ में कुछ दिन स्वास्थ्य सुधारने के लिए आ रहा है। मक्रील में जमी राष्ट्र-अभिमानी जनता, पलकों के पाँवड़े डाल उसकी अगवानी के लिए आतुर हो रही थी।
पहाड़ियों की छाती पर खिंची धूसर लकीर-सी सड़क पर धूल का एक बादल-सा दिखाई दिया। जनता की उत्सुक नजरें और उँगलियाँ उस ओर उठ गयीं। क्षण भर में धूल के बादल को फाड़ती हुई काले रंग की एक गतिमान वस्तु दिखाई दी। वह मोटर थी। आनन्द की हिलोर से जनता का समूह लहरा उठा। देखते ही देखते मोटर आ पहुँची।
जनता की उन्मत्तता के कारण मोटर को दस कदम पीछे ही रुक जाना पड़ा—‘देश के सिरताज की जय !’ सरस्वती के वरद पुत्र की जय !’ राष्ट्र के मुकुट-मणि की जय !’ के नारों से पहाड़ियाँ गूँज उठीं।
मोटर फूलों से भर गयी। बड़ी चहल-पहल के बाद जनता से घिरा हुआ, गजरों के बोझ से गर्दन झुकाए शनैः-शनैः कदम रखता हुआ मक्रील का अतिथि मोटर के अड्डे से चला।
उत्साह से बावली जनता विजयनाद करती हुई आगे-पीछे चल रही थी। जिन्होंने कवि का चेहरा देख पाया, वे भाग्यशाली विरले ही थे। ‘धवलगिरि’ होटल में दूसरी मंजिल पर कवि को टिकाने की व्यवस्था की गयी थी। वहाँ उसे पहुँचा, बहुत देर तक उसके आराम में व्याघात कर, जनता अपने स्थान को लौट आयी।
क्वार की त्रयोदशी का चन्द्रमा पार्वत्य-प्रदेश के निर्मल आकाश में ऊँचा उठ अपनी शीतल आभा से आकाश और पृथ्वी को स्तंभित किए हुए था। उस दूध की बौछार में ‘धवलिगिरि’ की हिमधवल दोमंज़िली इमारत चाँदी की दीवार-सी चमक रही थी। होटल के आँगन की फुलवारी में खूब चाँदनी थी, परन्तु उत्तर-पूर्व के भाग में इमारत के बाजू की छाया पड़ने से अँधेरा था। बिजली के प्रकाश से चमकती खिड़कियों के शीशों और पर्दों के पीछे से आने वाली मर्मध्वनि तथा नौकरों के चलने-फिरने की आवाज के अतिरिक्त सब शान्त था।
उस समय इस अँधेरे बाजू के नीचे के कमरे में रहने वाली एक युवती, फुलवारी के अन्धकारमय भाग में एक सरो के पेड़ के समीप खड़ी, दूसरी मंजिल में पुष्प-तोरणों से सजी उन खिड़कियों की ओर दृष्टि लगाये थी, जिनमें सम्मानित कवि को ठहराया गया था।
वह युवती भी उस आवेगमय स्वागत में सम्मिलित थी। पुलकित हो उसने ‘कवि’ पर फूल फेंके थे, जयनाद भी किया था। उस घमासान भीड़ में समीप पहुँच एक आँख के कवि देख लेने का अवसर उसे न मिला था। इसी साध को मन में लिये वह उस खिड़की की ओर टकटकी लगाए खड़ी थी। काँच पर कवि के शरीर की छाया उसे जब-तब दिखाई पड़ जाती।
स्फूर्तिप्रद भोजन के पश्चात कवि ने बरामदे में आ काले पहाडों के ऊपर चन्द्रमा के मोहक प्रकाश को देखा। सामने सँकरी धुँधली घाटी में बिजली की लपक की तरह फैली हुई मक्रील की धारा की ओर नजर गयी। नदी के प्रवाह की गम्भीर घरघराहट को सुन वह सिहर उठा। कितने ही क्षण मुँह उठाए वह मुग्ध भाव से खड़ा रहा। मक्रील नदी के उद्दाम प्रवाह के उस उज्ज्वल चाँदनी में देखने की इच्छा से कवि की आत्मा व्याकुल हो उठी। आवेश और उन्मेष का वह पुतला सौंदर्य के इस आह्वान की उपेक्षा न कर सका।
सरो वृक्ष के समीप खड़ी युवती पुलकित भाव से देश-कीर्ति के उस उज्ज्वल नक्षत्र को प्यासी आँखों से देख रही थी। चाँद के धुँधले प्रकाश में उसने इतनी दूर से उसने जो भी देख पाया, उसी से संतोष की साँस ले उसने श्रद्धा से सिर नवा दिया। इसे ही अपना सौभाग्य समझ वह चलने को थी कि लम्बा ओवरकोट पहने, छड़ी हाथ में लिये, दायीं ओर जीने से नीचे आता कवि दिखायी पड़ा। पल भर में कवि फुलवारी में आ पहुँचा।
फुलवारी में पहुँचने पर कवि को स्मरण हुआ, ख्यातनामा मक्रील नदी का मार्ग तो वह जानता ही नहीं। इस अज्ञान की अनुभूति से कवि ने दायें-बायें सहायता की आशा से देखा। समीप खडी़ एक युवती को देख, भद्रता से टोपी छूते हुए उसने पूछा—‘‘आप भी इस होटल में ठहरी हैं ?’’
सम्मान से सिर झुकाकर युवती ने उत्तर दिया—‘‘जी हाँ।’’
झिझकते हुए कवि ने पूछा—‘‘मक्रील नदी समीप ही किस ओर है, शायद आप जानती होंगी ?’’
उत्साह से कदम बढ़ाते हुई युवती बोली—‘‘जी हाँ। यही सौ कदम पर पुल है।’’
और मार्ग दिखाने के लिए वह प्रस्तुत हो गयी।
युवती के खुले मुख पर चन्द्रमा का प्रकाश पड़ रहा था। पतली भावों के नीचे बड़ी-बड़ी आँखों में मक्रील की उज्ज्वलता झलक रही थी।
कवि ने संकोच से कहा—‘‘न, न आपको व्यर्थ कष्ट होगा।’’
गौरव से युवती बोली—‘‘कुछ भी नहीं—यही तो है, सामने !’’
...उजली रात में संगमरमर की सुघड़ सुंदर सजीव मूर्ति-सी युवती...साहसमयी, विश्वासमयी मार्ग दिखाने चली सुन्दरता के याचक कवि को। कवि की कविता वीणा के सूक्ष्म तार स्पन्दित हो उठे...सुन्दरता स्वयं अपना परिचय देने चली...सृष्टि सौंदर्य के सरोवर की लहर उसे दूसरी लहर से मिलाने ले जा रही है—कवि ने सोचा।
सौ कदम पर मक्रील का पुल था। दो पहाड़ियों के तंग दर्रे में से उद्दाम वेग और घनघोर शब्द से बहते हुए जल के ऊपर तारों के रस्सों में झूलता हलका-सा पुल लटक रहा था। वे दोनों पुल के ऊपर जा खड़ा हुए। नीचे तीव्र वेग से लाखों-करोड़ों पिघले हुए चाँद बहते चले जा रहे थे, पार्श्व की चट्टानों से टकरा कर वे फेनिल हो उठते। फेनराशि से दृष्टि न हटा कवि ने कहा—‘‘सौंदर्य उन्मत्त हो उठा है।’’ युवती को जान पड़ा, मानो प्रकृति मुखरित हो उठी है।
कुछ क्षण पश्चात कवि बोला—‘‘आवेग में ही सौंदर्य का चरम विकास है। आवेग निकल जाने पर केवल कीचड़ रह जाता है।
युवती तन्मयता से उन सब्दों को पी रही थी। कवि ने कहा—‘‘अपने जन्म-स्थान पर मक्रील न इतनी वेगवती होगी, न इतनी उद्दा। शिशु की लटपट चाल से वह चलती होगी, समुद्र में पहुँच वह प्रौढ़ता की सिथिल गंभीरता धारण कर लेगी।’’
‘‘और मक्रील ! तेरा समय यही है। फूल न खिल जाने से पहले इतना सुन्दर होता है और न तब जब उसकी पँखुड़ियाँ लटक जायँ। उसका असली समय वही है, जब वह स्पुटोन्मुख हो। मधुमाखी उस समय पर निछावर होने के लिए मतवाली हो उठती है।’’ एक दीर्घ निःश्वास छो़ड़, आँखें झुका, कवि चुप हो गया।
मिनिट पर मिनिट गुजरने लगे। सर्द पहाड़ी हवा के झोंके से कवि के वृद्ध शरीर को समय का ध्यान आया। उसने देखा, मक्रील की फेनिल श्वेत, युवती की सुघड़ता पर विराज रही है। एक क्षण के लिए कवि, ‘‘घोर शब्दमयी प्रवाहमयी’ युवती को भूल मूक युवती का सौंदर्य निहारने लगा। हवा के दूसरे झोंके से सिहर कर वह बोला—‘‘समय अधिक हो गया है, चलना चाहिए।’’
लौटते समय मार्ग में कवि ने कहा—‘‘ आज त्रयोदशी के दिन यह शोभा है। कल और भी अधिक प्रकाश होगा। यदि असुविधा न हो तो क्या कल भी मारग दिखाने आओगी ?’’ और स्वयं ही संकोच के चाबुक की चोंट कर वह हँस पड़ा।
युवती ने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया—‘‘अवश्य।’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book









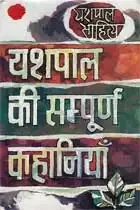


_s.webp)
