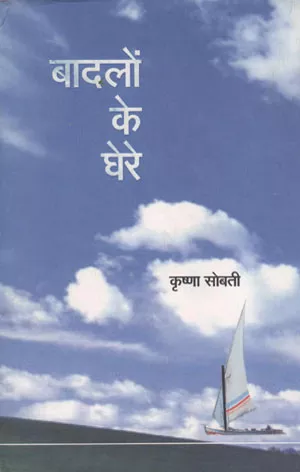|
कहानी संग्रह >> बादलों के घेरे बादलों के घेरेकृष्णा सोबती
|
158 पाठक हैं |
||||||
आधुनिक हिन्दी कथा-जगत में अपने विशिष्ट लेखन के लिए जानी जानेवाली वरिष्ठ लेखिका कृष्णा सोबती की प्रारम्भिक कहानियों का संकलन
Badlon Ke Ghere a hindi book by Krishna Sobti - बादलों के घेरे - कृष्णा सोबती
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
आधुनिक हिन्दी कथा-जगत में अपने विशिष्ट लेखन के लिए जानी जानेवाली वरिष्ठ लेखिका कृष्णा सोबती की प्रारम्भिक कहानियाँ इस पुस्तक में संकलित हैं।
शब्दों की आत्मा से साक्षात्कार करने वाली कृष्णा सोबती ने अपनी रचना-यात्रा के हर पड़ाव पर किसी-न-किसी सुखद विस्मय से हिन्दी-जगत् को रू-ब-रू कराया है।
ये कहानियाँ कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से कृष्णा जी के रचनात्मक वैविध्य को रेखांकित करती हैं। इनमें जीवन के विविध रंग और चेहरे अपनी जीवन्त उपस्थिति से समकालीन समाज के सच को प्रकट करते हैं। समय का सच इन कहानियों में इतनी व्यापकता के साथ अभिव्यक्त हुआ है कि आज के बदलते परिवेश में भी इनकी प्रासंगिकता बनी हुई है।
अनुभव की तटस्थता और सामाजिक परिवर्तन के द्वंद्व से उपजी ये कहानियाँ अपने समय और समाज को जिस आन्तरिकता और अंतरंगता से रेखांकित करती हैं वह निश्चय ही दुर्लभ है।
शब्दों की आत्मा से साक्षात्कार करने वाली कृष्णा सोबती ने अपनी रचना-यात्रा के हर पड़ाव पर किसी-न-किसी सुखद विस्मय से हिन्दी-जगत् को रू-ब-रू कराया है।
ये कहानियाँ कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से कृष्णा जी के रचनात्मक वैविध्य को रेखांकित करती हैं। इनमें जीवन के विविध रंग और चेहरे अपनी जीवन्त उपस्थिति से समकालीन समाज के सच को प्रकट करते हैं। समय का सच इन कहानियों में इतनी व्यापकता के साथ अभिव्यक्त हुआ है कि आज के बदलते परिवेश में भी इनकी प्रासंगिकता बनी हुई है।
अनुभव की तटस्थता और सामाजिक परिवर्तन के द्वंद्व से उपजी ये कहानियाँ अपने समय और समाज को जिस आन्तरिकता और अंतरंगता से रेखांकित करती हैं वह निश्चय ही दुर्लभ है।
बादलों के घेरे
भुवाली की एक छोटी सी कॉटेज में लेटा-लेटा मैं सामने के पहाड़ देखता हूँ। पानी भरे, सूखे-सूखे बादलों के घेरे देखता हूँ। बिना आँखों के भटक-भटक जाती धुन्ध के निष्फल प्रयास देखता हूँ। और फिर लेटे-लेटे अपने तन का पतझार देखता हूँ। सामने पहाड़ के रूखे हरियाले में रामगढ़ जाती हुई पगडंडी मेरी बाँह पर उभरी लम्बी नस की तरह चमकती है। पहाड़ी हवाएँ मेरी उखड़ी-उखड़ी साँस की तरह कभी तेज, कभी हौले इस खिड़की से टकराती हैं; पलंग पर बिछी चद्दर और ऊपर पड़े कम्बल से लिपटी मेरी देह चूने की सी कच्ची तह की तरह घुल-घुल जाती है और बरसों के ताने-बाने से बुनी मेरे प्राणों की धड़कने हर क्षण बन्द हो जाने के डर में चूक जाती हैं।
मैं लेटा रहता हूँ और सुबह हो जाती है। मैं लेटा रहता हूँ। शाम हो जाती है। मैं लेटा रहता हूँ, रात झुक जाती है। दरवाजे और खिड़कियों पर पड़े परदे मेरी ही तरह दिन-रात, सुबह-शाम अकेले मौन भाव से लटकते रहते हैं। कोई इन्हें भरे-भूरे हाथों से उठाकर कमरे की ओर बढ़ा नहीं जाता। रात, सुबह, शाम बारी-बारी से मेरी शैया के पास घिर घिर आते हैं और मैं अपनी इन फीकी आँखों से अँधेरे और उजाले को नहीं, लोहे के पलंग पर पड़े अपने आपको देखता हूँ। अपने इस छूटते-छूटते तन को देखता हूँ। और देखकर रह जाता हूँ। आज इस रह जाने के सिवाय कुछ भी मेरे वश में नहीं रह गया। सब अलग जा पड़ा है। अपने कन्धों से जुड़ी अपनी बाँहों को देखता हूँ, मेरी बाँहों में लगी वे भरी-भरी बाँहें-कहाँ हैं...कहां हैं वह सुगन्ध भरे केश जो मेरे वक्ष पर बिछ-बिछ जाते थे ? कहाँ हैं वे रस भरे अधर जो मेरे रस में भीग भीग जाते थे? सब था। मेरे पास सब था, बस, मैं आज सा नहीं था। जीने का संग था, सोने का संग था और उठने का संग था। मैं धुले-धुले सिरहाने पर सिर डालकर सोता रहता और कोई हौले से चूमकर कहता, ‘‘उठोगे नहीं..भोर हो गई!’’
आँखें बन्द किए-किए ही हाथ उस मोह-भरी देह को घेर लेते और रात के बीते क्षणों को सूँघ लेने के लिए अपनी ओर झुकाकर कहते, ‘‘इतनी जल्दी क्यों उठती हो’...
हल्की सी हँसी...और बाँहें खुल जातीं। आँखें खुल जातीं और गृहस्थी पर सुबह हो आती। फूलों की महक में नाश्ता लगता। धुले-ताजे कपड़ों में लिपटकर गृहस्थी की मालकिन अधिकार भरे संयम से सामने बैठ रात के सपने साकार कर देती। प्याले में दूध उँड़ेलती उन उँगलियों को देखता। क्या मेरे बालों को सहला-सहलाकर सिहरा देनेवाला स्पर्श इन्हीं की पकड़ में है ? आँचल को थामे आगे की ओर उठा हुआ कपड़ा जैसे दोनों ओर की मिठास को सम्हालने को सतर्क रहता। क्षण-भर को लगता, क्या गहरे में जो मेरा अपना है, यह उसके ऊपर का आवरण है या जो केवल मेरा है, वह इससे परे, इससे नीचे कहीं और है। एक शिथिल मगर बहती-बहती चाह विभोर कर जाती। मैं होता, मुझसे लगी एक और देह होती। उसमें मिठास होती, जो रात में लहरा-लहरा जाती। और एक रात भुवाली के इस क्षय-ग्रस्त अँधियारे में आती है। कम्बल के नीचे पड़ा-पड़ा मैं दवा की शीशियाँ देखता हूँ और उन पर लिखे विज्ञापन देखता हूँ। घूँट भरकर जब इन्हें पीता हूँ, तो सोचता हूँ, तन के रस रीत जाने पर हाड़-मांस सब काठ हो जाते हैं। मिट्टी नहीं कहता हूँ। मिट्टी हो जाने से तो मिट्टी से फिर रस उभरता है, अभी तो मुझे मिट्टी होना है।
कैसे सरसते दिन थे ! तन-मन को सहलाते-बहलाते उस एक रात को मैं आज के इस शून्य में टटोलता हूँ। सर्दियों के एकान्त मौन में एकाएक किसी का आदेश पाकर मैं कमरे की ओर बढ़ता हूँ। बल्ब के नीले प्रकाश में दो अधखुली थकी-थकी पलकें जरा-सी उठती हैं और बाँह के घेरे तले सोये शिशु को देखकर मेरे चेहरे पर ठहर जाती हैं। जैसी कहती हों-तुम्हारे आलिंगन को तुम्हारा ही तन देकर सजीव कर दिया है। मैं उठता हूँ, ठंडे मस्तक को अधरों से छूकर यह सोचते-सोचते उठता हूँ कि जो प्यार तन में जगता है, तन से उपजता है, वही देह पाकर दुनिया में जी भी जाता है।
पर कहीं, एक दूसरा प्यार भी होता है, जो पहाड़ के सूखे बादलों की तरह उठ-उठ आता है, और बिना बरसे ही भटक-भटककर रह जाता है।
वर्षों बीते। एक बार गर्मी में पहाड़ गया था। बुआ के यहाँ पहली बार उन आँखों-सी आँखों को देखा था। धुपाती सुबह थी। नाश्ते की मेज से उठा, तो परिचय करवाते-करवाते न जाने क्यों बुआ का स्वर जरा सा अटका था...साँस लेकर कहा, ‘‘मन्नो से मिलो रवि, दो ही दिन यहाँ रुकेगी।’’ बुआ के मुख से यह फीका परिचय अच्छा नहीं लगा। साँस भरकर बुआ का वह दो दिन कहना किसी कड़ेपन को झेल लेने सा लगा। वह कुछ बोली नहीं। सिर हिलाकर अभिवादन का उत्तर दिया और जरा सा हँस दी। उस दूर-दूर लगनेवाले चेहरे से मैं अपने को लौटा नहीं सका। उस पतले, किन्तु भरे-भरे मुख पर कसकर बाँधे घुँघराले बालों को देखकर मन में कुछ ऐसा सा हो आया कि किसी ने गहरे उलाहने की सजा अपने को दे डाली है।
सब उठकर बाहर आए, तो बुआ के बच्चे उस दुबली देह पर खड़े आँचल को खींच स्नेहवश उन बाँहों से लिपट-लिपट गए-मन्नो जीजी....मन्नो जीजी। बुआ किसी काम से अन्दर जा रही थीं, खिलखिलाहट सुनकर लौट पड़ीं। बुआ का वह कठिन, बँधा और खिंचावट को छिपानेवाले चेहरा मैं आज भी भूला नहीं हूँ। कड़े हाथों से बच्चों को छुड़ाती ठंडी निगाह से मन्नो को देखती हुई ढीले स्वर में बोली, ‘‘जाओ मन्नो कहीं घूम आओ। तुम्हें उलझा-उलझाकर तो ये बच्चे तंग कर डालेंगे।’’..माँ की घुड़की आँखों-ही-आँखों में समझकर बच्चे एक ओर हो गए। बुआ के खाली हाथ जैसे झेंपकर नीचे लटक गए और मन्नो की बड़ी-बड़ी आँखों की घनी पलकें न उठीं, न गिरी, बस एकटक बुआ की ओर देखती रह गईं...
बुआ इस संकोच से उबरी, तो मन्नो धीमी गति से फाटक से बाहर हो गई थी। कुछ समझ लेने के लिए आग्रह से बुआ से पूछा, ‘कहो तो बुआ, बात क्या है?’’
बुआ अटकी, फिर झिझककर बोली, ‘‘बीमार है रवि, दो बरस सैनेटोरियम में रहने के बाद अब जेठजी ने वहीं कॉटेज ले दी है। साथ घर का पुराना नौकर रहता है। कभी अकेले जी ऊब जाता है, तो दो चार दिन को शहर चली जाती है।’’
‘‘नहीं नहीं बुआ !’’ मैं धक्का खाकर जैसे विश्वास नहीं करना चाहता।
‘‘रवि, जब कभी चार-छह महीने बाद लड़की को देखती हूँ, तो भूख-प्यास सब सूख जाती है।’’
मैं बुआ की इस सच्चाई को कुरेद लेने को कहता हूँ, ‘‘बुआ, बच्चों को एकदम अलग करना ठीक नहीं हुआ, पल-भर तो रुक जाती।’’
बुआ ने बहुत कड़ी निगाह से देखा, जैसा कहना चाहती हो, ‘तुम यह सब नहीं समझोगे’ और अन्दर चली गई। बच्चे अपने खेल में जुट गए थे। मैं खड़ा-खड़ा बार-बार सिगरेट के धुएँ से अपने तन का भय और मन की जिज्ञासा उड़ाता रहा। कितनी घुटन होगी उन प्राणों में ! पर हुआ भी तो कुछ गलत नहीं था। उलझा-उलझा सा मैं बाहर निकला और उतराई उतरकर झील के किनारे-किनारे हो गया। सड़क के साथ-साथ इस ओर छाँह थी। उछल-उछल आती पानी की लहरें कभी धूप से रुपहली हो जाती थीं। देवी के मन्दिर के आगे पहुँचा, तो रुका, जँगले पर हाथ टिकाए झील में नौकाओं की दौड़ देखता रहा। बलिष्ठ हाथों में चप्पू थामे कुछ युवक तेज रफ्तार तल्लीताल की ओर जा रहे हैं, पीछे की किश्ती में अपने तन-मन से बेखबर एक प्रौढ़ बैठा ऊँघ रहा है। उसके पीछे बोट-क्लब की किश्ती में विदेशी युवतियाँ...फिर और दो-चार पालवाली नौकाएँ...
एकाएक किश्ती में नहीं, जैसे पानी की नीची सतह पर वही पीला चेहरा देखता हूँ, वही बड़ी-बड़ी आँखें, वही दुबली-पतली बाँहें, वही बुआ की घरवाली मन्नो। दो-चार बार मन-ही-मन नाम दोहराता हूँ, मन्नो, मन्नो, मन्नो.... लगता है मैं ऊँचे किनारे पर खड़ा हूँ और पानी के साथ साथ मन्नो बही चली जा रही है। खिंचे घुँघराले बाल, अनझपी, पलकें...पर बुआ कहती थी बीमार है, मन्नो बीमार है।
जँगले पर से हाथ उठाकर बुआ के घर की दिशा में देखता हूँ। चीना की चोटी अपने पहाड़ी संयम से सिर उठाए सदा की तरह सीधी खड़ी है। एक ढलती-सी पथरीली ढलान को उसने जैसे हाथ से थाम रखा है। और मैं नीचे इस सड़क पर खड़े सोचता हूँ कि सब कुछ रोज जैसा है, केवल मन से उभर-उभर आती वे दो आँखें नई हैं और उन दो आँखों के पीछे की बीमारी....जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई उबार नहीं सकता।
घर पहुचा, तो बुआ बच्चों को लेकर कहीं बाहर चली गई थी। कुछ देर ड्राइंग-रूम में बैठा-बैठा बुआ के सुघड़ हाथों द्वारा की गई सजावट को देखता रहा। कीमती फूलदानों में लगाई गई पहाड़ी झाड़ियाँ सुन्दर लगती थीं। कैबिनेट पर बड़ी कीमती फ्रेम में लगे सपरिवार चित्र के आगे खड़ा हुआ, तो बुआ के साथ खड़े फूफा की ओर देखकर सोचता रहा कि बुआ के लिए इस चेहरे पर कौन सा आकर्षण है, जिससे बँधी-बँधी वह दिन रात, वर्ष मास अपने को निभाती चली आती है, पर नहीं बुआ के ही घर में होकर यह सोचना मन के शील से परे है...
झिझककर ड्राइंग रूम से निकलता हूँ और अपने कमरे की सीढ़ियाँ चढ़ जाता हूँ। सिगरेट जलाकर झील के दक्खिनी किनारे पर खुलती खिड़की के बाहर देखने लगता हूँ। हरे पहाड़ों के छोटे-बड़े आकारों में टीन की लाल-लाल छतें और बीच-बीच में मटियाली पगडंडियाँ। बुआ खाने तक लौट आएँगी और मन्नो भी तो...देर तक बैठा-बैठा किसी पुराने अखबार के पन्ने पलटता रहा। बुआ लौटी नहीं। घड़ी की टन-टन के साथ नौकर ने खाने के लिए अनुरोध किया।
‘‘खाना लगेगा, साहिब ?’’
‘‘बुआ कब तक लौटेंगी ?’’
‘‘खाने को तो मना कर गई हैं।’’
कथन के रहस्य को मैं इन अर्थहीन सी आँखों में पढ़ जाने के प्रयत्न में रहता हूँ।
‘‘और जो मेहमान हैं ?’’
नौकर तत्परता से झुककर बोला, ‘‘आपके साथ नहीं, साहिब! वह अलग से ऊपर खाएँगी।’’
मैं एक लम्बी साँस भरकर जले सिगरेट के टुकड़े को पैर के नीचे कुचल देता हूँ। शायद साथ खाने के डर से छुटकारा पाने पर या शायद साथ न खा सकने की विवशता पर। उस खाने की मेज पर अकेले खाना खाते-खाते क्या सोचता रहा था, आज तो याद नहीं, बस इतना-सा याद है, काँटे-छुरी से उलझता बार-बार मैं बाहर की ओर देखता था।
मीठा कौर मुँह में लेते ही घोड़े की टाप सुनाई दी, ठिठककर सुना, ‘‘सलाम, साहिब।’’
धीमी मगर सधी आवाज, ‘‘दो घंटे तक पहुँच सकोगे न ?’’
‘‘जी, हुजूर। ’’
सीढ़ियों पर आहट हुई और शायद अपने कमरे तक पहुँचकर खत्म हो गई। खाने के बरतन उठ गए। मैं उठा नहीं। दोबारा कॉफी पी लेने के बाद भी वहीं बैठा रहा। एकाएक मन में आया कि किसी के छोटे से परिचय से मन में इतनी दुविधा उपजा लेना कम छोटी दुर्बलता नहीं है। आखिर किसी से मिल ही लिया हूँ, तो उसके लिए ऐसा-सा क्यों हुआ जा रहा हूँ।
घंटे-भर बाद मैं किसी की पैरों चली सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ा जा रहा था। खुले द्वार पर परदा पड़ा था। हौले से थाप दी।
‘‘चले आइए।’’
परदा उठाकर देहरी पर पाँव रखा। हाथ में कश्मीरी शॉल लिये मन्नो सूटकेस के पास खड़ी थी। देखकर चौंकी नहीं। सहज स्वर में कहा, ‘‘आइए।’’ फिर सोफे पर फैले कपड़े उठाकर कहा, ‘‘बैठिए।’’
बैठते-बैठता सोचा, बुआ के घर भर में सबसे अधिक सजा और साफ कमरा यही है। नया-नया फर्नीचर, कीमती परदे और इन सबमें हल्के पीले कपड़ों में लिपटी मन्नो। अच्छा लगा।
बात करने को कुछ भी न पाकर बोला, ‘‘आप लंच तो...’’
‘‘जी, मैं कर चुकी हूँ।’’ और भरपूर मेरी ओर देखती रही।
मैं जैसे कुछ कहलवा लेने को कहता हूँ, ‘‘बुआ तो कहीं बाहर गई हैं।’’
सिर हिलाकर मन्नो शॉल की तह लगाती है और सूटकेस में रखते-रखते कहती है, ‘‘शाम से पहले ही नीचे उतर जाऊँगी। बुआ से कहिएगा एक ही दिन को आई थी।’’
‘‘बुआ तो आती ही होंगी।’’
इसका उत्तर न शब्दों में आया, न चेहरे पर से। कहते-कहते एक बार रुका, फिर न जाने कैसे आग्रह से कहा, ‘‘एक दिन और नहीं रुक सकेंगी !’’
वह कुछ बोली नहीं। बन्द करते सूटकेस पर झुकी रही।
फिर पल-भर बाद जैसे स्नेह भरे हाथ से अपने बालों को छुआ और हँसकर कहा, ‘‘क्या करूँगी यहाँ रहकर ? भुवाली के इतने बड़े गाँव के बाद यह छोटा सा शहर मन को भाता नहीं।’’
वह छोटी सी खिलखिलाहट, वह कड़वाहट से परे का व्यंग्य, आज इतने वर्षों के बाद भी, मैं वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही सुन रहा हूँ। वही शब्द हैं, वही हँसी और वही पीली-सी सूरत...
हम संग-संग नीचे उतरे थे। मेरी बाँह पर मन्नो का कोट था। नौकर और माली ने झुककर सलाम किया और अतिथि से इनाम पाया। साईस ने घोड़े को थपथपाया।
‘‘हुजूर चढ़ेगी।’’
उड़ती-उड़ती नजर उन आँखों की, बाँह पर लटके कोट पर अटकी।
‘‘पैदल जाऊँगी। घोड़ा आगे-आगे लिए चलो।’’
चाहा कि घोड़े पर चढ़ जाने के लिए अनुरोध करूँ, पर कह नहीं पाया। फाटक से बाहर होते-होते वह पल-भर को पीछे मुड़ी, जैसे छोड़ने के पहले घर को देखती हो। फिर एकाएक अपने को सँभालकर नीचे उतर गई।
टैक्सी खड़ी थी। सामान लदा। ड्राइवर ने उन कठिन क्षणों को मानो भाँपकर कहा, ‘‘कुछ और देर है, साहिब।’’
मन्नो ने इस बार कहीं देखा नहीं। कोट लेने के लिए मेरी ओर हाथ बढ़ा दिया। कार में बैठी तो कुली ने तत्परता से पीछे से कम्बल निकाला और घुटनों पर डालते हुए कहा, ‘‘कुछ, और मेम साहिब ?’’
घुँघराली छाँह ढीली-सी होकर सीट के साथ जा टिकी। घुटनों पर पतली-पतली सी विवश बाँहें फैलाते हुए धीरे से कहा, ‘‘नहीं-नहीं, कुछ और नहीं। धन्यवाद।’’
अधखुले काँच में से अन्दर झाँका। मुख पर थकान के चिह्न थे। बाँहों में मछलीमुखी कंगन थे। आँखों में, क्या था, यह मैं पढ़ नहीं पाया। वही पीली, पतझड़ी दृष्टि उन हाथों पर जमी थी, जो कम्बल पर एक-दूसरे से लगे मौन पड़े थे।
कार स्टार्ट हुई। मैं पीछे हटा और कार चल दी। विदाई के लिए न हाथ उठे, न अधर हिले। मोड़ तक पहुँचने तक पीछे के शीशे से सादगी से बँधा बालों का रिबन देखता रहा और देर तक वह दर्दीले धन्यवाद की गूँज सुनता रहा-नहीं-नहीं, कुछ और नहीं।
वे पल अपनी कल्पना से आज भी लौटता हूँ तो जी को कुछ होने लगता है। उस कार को भगा ले जानेवाली सूखी सड़क से घूमकर मैं ताल के किनारे-किनारे चला जा रहा हूँ। अपने को समझाने-बुझाने पर भी वह चेहरा, वह बीमारी मन पर से नहीं उतरती। रुक-रुककर, थक-थककर जैसे मैं उस दिन घर की चढ़ाई चढ़ा था, उसे याद कर आज भी निढाल हो जाता हूँ। घर पहुँचा। बरामदे में से कुली फर्नीचर निकाल रहे थे। मन धक्का खाकर रह गया। तो उस मन्नो के कमरे की सजावट, सुख-सुविधा सब किराए पर बुआ ने जुटाए थे। दुपहर में बुआ के प्रति जो कुछ जितना भी अच्छा लगा था, वह सब उल्टा हो गया।
आगे बढ़ा, तो द्वार पर बुआ खड़ी थीं। सन्देह से मुझे देख और पास होकर फीके गले से कहा, ‘रवि, मुँह हाथ धो डालो, सामान सब तैयार मिलेगा वहाँ, जल्दी लौटोगे न, चाय लगने को ही है !’’
चुपचाप बाथरूम में पहुँच गया। सामान सब था। मुँह-हाथ धोने से पहले गिलास में ढँककर रखे गर्म पानी से गला साफ किया। ऐसा लगा, किसी की घुटी-घुटी जकड़ में से बाहर निकल आया हूँ। कपड़े बदलकर चाय पर जा बैठा। बच्चे नहीं, केवल बुआ थीं। बुआ ने चाय उँड़ेली और प्याला आगे कर दिया।
‘‘बुआ !’’
बुआ ने जैसे सुना नहीं।
‘‘बुआ, बुआ !’’-पल-भर के लिए अपने को ही कुछ ऐसा सा लगा कि किसी और को पुकारने के लिए बुला को पुकार रहा हूँ। बुआ ने विवश हो आँखें ऊपर उठाईं। समझ गया कि बुआ चाहती हैं, कुछ कहूँ नहीं, पर मैं रुका नहीं।
‘‘बुआ दो दिन की मेहमान तो एक ही दिन में चली गई।’’
सुनकर बुआ चम्मच से अपनी चाय हिलाने लगीं। कुछ बोली नहीं। इस मौन से मैं और भी निर्दयी हो गया।
‘‘कहती थी, बुआ से कहना मैं एक ही दिन को आई थी।’’
इसके आगे बुआ जैसे कुछ और सुन नहीं सकीं। गहरा लम्बा श्वास लेकर आहत आँखों से मुझे देखा, ‘‘तुम कुछ और नहीं कहोगे, रवि....’’ और चाय का प्याला वहीं छोड़ कमरे से बाहर हो गईं।
उस रात दौरे से फूफा के लौटने की बात थी। नौकर से पूछा तो पता लगा, दो दिन के बाद आने का तार आ चुका है। चाहा, एक बार बुआ के कमरे तक हो आऊँ, पर संकोचवश पाँव उठे नहीं। देर बाद सीढ़ियों में अपने को पाया, तो सामने मन्नो का खाली कमरा था। आगे बढ़कर बिजली जलाई, सब खाली था, न परदे, न फर्नीचर...न मन्नो...एकाएक अँगीठी में लगी लकड़ियों को देख मन में आया, आज वह यहाँ रहती, तो रात देर गए इसके पास यहीं बैठी रहती और मैं शायद इसी तरह जैसे अब यहाँ आया हूँ, उसके पास आता, उसके...
यह सब मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ...
किसी अनदेखे भय से घबराकर नीचे उतर आया। खिड़की से बाहर देखा, अँधेरा था। सिरहाना खींचा, बिजली बुझाई और बिस्तर पर पड़े-पड़े भुवाली की वह छोटी सी कॉटेज देखता रहा, जहाँ अब तक मन्नो पहुँच गई होगी।
‘‘रवि !’’
मैं चौंका नहीं, यह बुआ का स्वर था। बुआ अँधेरे में ही पास आ बैठीं और हौले-हौले सिर सहलाती रहीं।
‘‘बुआ।’’
बुआ का हाथ पल-भर को थमा फिर कुछ झुककर मेरे माथे तक आ गया। रुँधे स्वर से कहा, ‘‘रवि, तुम्हें नहीं, उस लड़की को दुलराती हूँ। अब यह हाथ उस तक नहीं पहुँचता...’’
मैं बुआ का नहीं, मन्नो का हाथ पकड़ लेता हूँ।
बुआ देर तक कुछ नहीं बोलीं। फिर जैसे कुछ समझते हुए अपने को कड़ा कर कहा, ‘‘रवि, उसके लिए कुछ मत सोचो, उसे अब रहना नहीं है।’’
मैं बुआ के स्पर्श तले सिहरकर कहता हूँ, ‘‘बुआ, मुझे ही कौन रहना है ?’’
आज वर्षों बाद भुवाली में पड़े-पड़े मैं असंख्य बार सोचता हूँ कि उस रात मैं अपने लिए यह क्यों कह गया था ! क्यों कह गया था वे अभिशाप के बोल, जो दिन-रात मेरे इस तन-मन पर से सच्चे उतरे जा रहे हैं ? सुनकर बुआ को कैसा लगा, नहीं जानता। वे हाथ खींचकर उठीं। रोशनी की, और पूरी आँखों से मुझे देखकर अविश्वास और भर्त्सना से कहा, ‘‘पागल हो गए हो, रवि ! उसके साथ अपनी बात जोड़ते हो, जिसके लिए कोई राह नहीं रह गई, कोई और राह नहीं रह गई।’’
फिर कुर्सी पर बैठते-बैठते कहा, ‘‘रवि, तुम तो उसे सुबह-शाम तक ही देख पाए हो। मैं वर्षों से उसे देखती आई हूँ और आज पत्थर-सी निष्ठुर हो गई हूँ। उसे अपना बच्चा ही करके मानती रही हूँ, यह नहीं कहूँगी। अपने बच्चों की तरह तो अपने बच्चों के सिवाय और किस रखा जा सकता है ! पर जो कुछ जितना भी था, वह प्यार वह देखभाल सब व्यर्थ हो गए हैं। कभी छुट्टी के दिन उसका बोर्डिग से आने की राह तकती थी, अब उसके आने से पहले उसके जाने का क्षण मनाती हूँ और डरकर बच्चों को लिये घर से बाहर निकल जाती हूँ।’’
बुआ के बोल कठिन हो आए।
‘‘रवि, जिसे बचपन में मोहवश कभी डराना नहीं चाहती थी, आज उसी से डरने लगी हूँ। उसकी बीमारी से डरने लगी हूँ।’’ फिर स्वर बदलकर कहा, ‘‘तुम्हारा ऐसा जीवट मुझमें नहीं कि कहूँ, डरती हूँ।’’ बुआ ने यह कहकर जैसे मुझे टटोला-और मैं बिना हिलेडुले चुपचाप लेटा रहा।
बुआ असमंजस में देर तक मुझे देखती रहीं। फिर जाने को उठीं और और रुक गईं। इस बार स्वर में आग्रह नहीं, चेतावनी थी, ‘‘रवि, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जिसके लिए सब राह रुकी हों, उसके लिए भटको नहीं।’’
पर उस दिन बुआ की बात मैं समझा नहीं, चाहने पर भी नहीं।
अगली सुबह चाहा कि घूम-घूमकर दिन बिता दूँ। घोड़ा दौड़ाता लड़ियाकाँटा पहुँचा और उन्हीं पैरों लौट आया। घर की ओर मुँह करते करते, न जाने क्यों, मन को कुछ ऐसा लगा कि मुझे घर नहीं, कहीं और पहुँचना है। चढ़ाई के मोड़ पर कुछ देर खड़ा-खड़ा सोचता रहा और जब ढलती दुपहरी में तल्लीताल की उतराई उतरा तो मन के आगे सब साफ था।
मुझे भुवाली जाना था।
बस से उतरा। अड्डे पर रामगढ़ के लाल-लाल सेबों के ढेर देखकर यह नहीं लगा कि यही भुवाली है। बस में सोचता आया था कि वहाँ घुटन होगी; पर चीड़ के ऊँचे-ऊँचे पेड़ों से लहराती हवाएँ बह-बह आती थीं। छाँह ऊपर उठती है, धूप नीचे उतरती है और भुवाली मन को अच्छी लगती है। तन को अच्छी लगती है। चौराहे से होकर पोस्ट-ऑफिस पहुँचा। कॉटेज का पता लगा लिया और छोटे से पहाड़ी बाजार में होता हुआ ‘पाइंस’ की ओर हो लिया। खुली-चौड़ी सड़क के मोड़ से अच्छी सी पतली राह ऊपर जा रही थी। जँगले से नीचे देखा, अलग-अलग खड़े पहाड़ों के बीच की जगह पर एक खुली-चौड़ी घाटी बिछी थी। तिरछे-सीछे, खेत किसी के घुटने पर रखे कसीदे के कपड़े की तरह धरती पर फैले थे। दूर सामने दक्खिन की ओर पानी का ताल धूप में चाँदी के थाल की तरह चमकता था।
मैं लेटा रहता हूँ और सुबह हो जाती है। मैं लेटा रहता हूँ। शाम हो जाती है। मैं लेटा रहता हूँ, रात झुक जाती है। दरवाजे और खिड़कियों पर पड़े परदे मेरी ही तरह दिन-रात, सुबह-शाम अकेले मौन भाव से लटकते रहते हैं। कोई इन्हें भरे-भूरे हाथों से उठाकर कमरे की ओर बढ़ा नहीं जाता। रात, सुबह, शाम बारी-बारी से मेरी शैया के पास घिर घिर आते हैं और मैं अपनी इन फीकी आँखों से अँधेरे और उजाले को नहीं, लोहे के पलंग पर पड़े अपने आपको देखता हूँ। अपने इस छूटते-छूटते तन को देखता हूँ। और देखकर रह जाता हूँ। आज इस रह जाने के सिवाय कुछ भी मेरे वश में नहीं रह गया। सब अलग जा पड़ा है। अपने कन्धों से जुड़ी अपनी बाँहों को देखता हूँ, मेरी बाँहों में लगी वे भरी-भरी बाँहें-कहाँ हैं...कहां हैं वह सुगन्ध भरे केश जो मेरे वक्ष पर बिछ-बिछ जाते थे ? कहाँ हैं वे रस भरे अधर जो मेरे रस में भीग भीग जाते थे? सब था। मेरे पास सब था, बस, मैं आज सा नहीं था। जीने का संग था, सोने का संग था और उठने का संग था। मैं धुले-धुले सिरहाने पर सिर डालकर सोता रहता और कोई हौले से चूमकर कहता, ‘‘उठोगे नहीं..भोर हो गई!’’
आँखें बन्द किए-किए ही हाथ उस मोह-भरी देह को घेर लेते और रात के बीते क्षणों को सूँघ लेने के लिए अपनी ओर झुकाकर कहते, ‘‘इतनी जल्दी क्यों उठती हो’...
हल्की सी हँसी...और बाँहें खुल जातीं। आँखें खुल जातीं और गृहस्थी पर सुबह हो आती। फूलों की महक में नाश्ता लगता। धुले-ताजे कपड़ों में लिपटकर गृहस्थी की मालकिन अधिकार भरे संयम से सामने बैठ रात के सपने साकार कर देती। प्याले में दूध उँड़ेलती उन उँगलियों को देखता। क्या मेरे बालों को सहला-सहलाकर सिहरा देनेवाला स्पर्श इन्हीं की पकड़ में है ? आँचल को थामे आगे की ओर उठा हुआ कपड़ा जैसे दोनों ओर की मिठास को सम्हालने को सतर्क रहता। क्षण-भर को लगता, क्या गहरे में जो मेरा अपना है, यह उसके ऊपर का आवरण है या जो केवल मेरा है, वह इससे परे, इससे नीचे कहीं और है। एक शिथिल मगर बहती-बहती चाह विभोर कर जाती। मैं होता, मुझसे लगी एक और देह होती। उसमें मिठास होती, जो रात में लहरा-लहरा जाती। और एक रात भुवाली के इस क्षय-ग्रस्त अँधियारे में आती है। कम्बल के नीचे पड़ा-पड़ा मैं दवा की शीशियाँ देखता हूँ और उन पर लिखे विज्ञापन देखता हूँ। घूँट भरकर जब इन्हें पीता हूँ, तो सोचता हूँ, तन के रस रीत जाने पर हाड़-मांस सब काठ हो जाते हैं। मिट्टी नहीं कहता हूँ। मिट्टी हो जाने से तो मिट्टी से फिर रस उभरता है, अभी तो मुझे मिट्टी होना है।
कैसे सरसते दिन थे ! तन-मन को सहलाते-बहलाते उस एक रात को मैं आज के इस शून्य में टटोलता हूँ। सर्दियों के एकान्त मौन में एकाएक किसी का आदेश पाकर मैं कमरे की ओर बढ़ता हूँ। बल्ब के नीले प्रकाश में दो अधखुली थकी-थकी पलकें जरा-सी उठती हैं और बाँह के घेरे तले सोये शिशु को देखकर मेरे चेहरे पर ठहर जाती हैं। जैसी कहती हों-तुम्हारे आलिंगन को तुम्हारा ही तन देकर सजीव कर दिया है। मैं उठता हूँ, ठंडे मस्तक को अधरों से छूकर यह सोचते-सोचते उठता हूँ कि जो प्यार तन में जगता है, तन से उपजता है, वही देह पाकर दुनिया में जी भी जाता है।
पर कहीं, एक दूसरा प्यार भी होता है, जो पहाड़ के सूखे बादलों की तरह उठ-उठ आता है, और बिना बरसे ही भटक-भटककर रह जाता है।
वर्षों बीते। एक बार गर्मी में पहाड़ गया था। बुआ के यहाँ पहली बार उन आँखों-सी आँखों को देखा था। धुपाती सुबह थी। नाश्ते की मेज से उठा, तो परिचय करवाते-करवाते न जाने क्यों बुआ का स्वर जरा सा अटका था...साँस लेकर कहा, ‘‘मन्नो से मिलो रवि, दो ही दिन यहाँ रुकेगी।’’ बुआ के मुख से यह फीका परिचय अच्छा नहीं लगा। साँस भरकर बुआ का वह दो दिन कहना किसी कड़ेपन को झेल लेने सा लगा। वह कुछ बोली नहीं। सिर हिलाकर अभिवादन का उत्तर दिया और जरा सा हँस दी। उस दूर-दूर लगनेवाले चेहरे से मैं अपने को लौटा नहीं सका। उस पतले, किन्तु भरे-भरे मुख पर कसकर बाँधे घुँघराले बालों को देखकर मन में कुछ ऐसा सा हो आया कि किसी ने गहरे उलाहने की सजा अपने को दे डाली है।
सब उठकर बाहर आए, तो बुआ के बच्चे उस दुबली देह पर खड़े आँचल को खींच स्नेहवश उन बाँहों से लिपट-लिपट गए-मन्नो जीजी....मन्नो जीजी। बुआ किसी काम से अन्दर जा रही थीं, खिलखिलाहट सुनकर लौट पड़ीं। बुआ का वह कठिन, बँधा और खिंचावट को छिपानेवाले चेहरा मैं आज भी भूला नहीं हूँ। कड़े हाथों से बच्चों को छुड़ाती ठंडी निगाह से मन्नो को देखती हुई ढीले स्वर में बोली, ‘‘जाओ मन्नो कहीं घूम आओ। तुम्हें उलझा-उलझाकर तो ये बच्चे तंग कर डालेंगे।’’..माँ की घुड़की आँखों-ही-आँखों में समझकर बच्चे एक ओर हो गए। बुआ के खाली हाथ जैसे झेंपकर नीचे लटक गए और मन्नो की बड़ी-बड़ी आँखों की घनी पलकें न उठीं, न गिरी, बस एकटक बुआ की ओर देखती रह गईं...
बुआ इस संकोच से उबरी, तो मन्नो धीमी गति से फाटक से बाहर हो गई थी। कुछ समझ लेने के लिए आग्रह से बुआ से पूछा, ‘कहो तो बुआ, बात क्या है?’’
बुआ अटकी, फिर झिझककर बोली, ‘‘बीमार है रवि, दो बरस सैनेटोरियम में रहने के बाद अब जेठजी ने वहीं कॉटेज ले दी है। साथ घर का पुराना नौकर रहता है। कभी अकेले जी ऊब जाता है, तो दो चार दिन को शहर चली जाती है।’’
‘‘नहीं नहीं बुआ !’’ मैं धक्का खाकर जैसे विश्वास नहीं करना चाहता।
‘‘रवि, जब कभी चार-छह महीने बाद लड़की को देखती हूँ, तो भूख-प्यास सब सूख जाती है।’’
मैं बुआ की इस सच्चाई को कुरेद लेने को कहता हूँ, ‘‘बुआ, बच्चों को एकदम अलग करना ठीक नहीं हुआ, पल-भर तो रुक जाती।’’
बुआ ने बहुत कड़ी निगाह से देखा, जैसा कहना चाहती हो, ‘तुम यह सब नहीं समझोगे’ और अन्दर चली गई। बच्चे अपने खेल में जुट गए थे। मैं खड़ा-खड़ा बार-बार सिगरेट के धुएँ से अपने तन का भय और मन की जिज्ञासा उड़ाता रहा। कितनी घुटन होगी उन प्राणों में ! पर हुआ भी तो कुछ गलत नहीं था। उलझा-उलझा सा मैं बाहर निकला और उतराई उतरकर झील के किनारे-किनारे हो गया। सड़क के साथ-साथ इस ओर छाँह थी। उछल-उछल आती पानी की लहरें कभी धूप से रुपहली हो जाती थीं। देवी के मन्दिर के आगे पहुँचा, तो रुका, जँगले पर हाथ टिकाए झील में नौकाओं की दौड़ देखता रहा। बलिष्ठ हाथों में चप्पू थामे कुछ युवक तेज रफ्तार तल्लीताल की ओर जा रहे हैं, पीछे की किश्ती में अपने तन-मन से बेखबर एक प्रौढ़ बैठा ऊँघ रहा है। उसके पीछे बोट-क्लब की किश्ती में विदेशी युवतियाँ...फिर और दो-चार पालवाली नौकाएँ...
एकाएक किश्ती में नहीं, जैसे पानी की नीची सतह पर वही पीला चेहरा देखता हूँ, वही बड़ी-बड़ी आँखें, वही दुबली-पतली बाँहें, वही बुआ की घरवाली मन्नो। दो-चार बार मन-ही-मन नाम दोहराता हूँ, मन्नो, मन्नो, मन्नो.... लगता है मैं ऊँचे किनारे पर खड़ा हूँ और पानी के साथ साथ मन्नो बही चली जा रही है। खिंचे घुँघराले बाल, अनझपी, पलकें...पर बुआ कहती थी बीमार है, मन्नो बीमार है।
जँगले पर से हाथ उठाकर बुआ के घर की दिशा में देखता हूँ। चीना की चोटी अपने पहाड़ी संयम से सिर उठाए सदा की तरह सीधी खड़ी है। एक ढलती-सी पथरीली ढलान को उसने जैसे हाथ से थाम रखा है। और मैं नीचे इस सड़क पर खड़े सोचता हूँ कि सब कुछ रोज जैसा है, केवल मन से उभर-उभर आती वे दो आँखें नई हैं और उन दो आँखों के पीछे की बीमारी....जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई उबार नहीं सकता।
घर पहुचा, तो बुआ बच्चों को लेकर कहीं बाहर चली गई थी। कुछ देर ड्राइंग-रूम में बैठा-बैठा बुआ के सुघड़ हाथों द्वारा की गई सजावट को देखता रहा। कीमती फूलदानों में लगाई गई पहाड़ी झाड़ियाँ सुन्दर लगती थीं। कैबिनेट पर बड़ी कीमती फ्रेम में लगे सपरिवार चित्र के आगे खड़ा हुआ, तो बुआ के साथ खड़े फूफा की ओर देखकर सोचता रहा कि बुआ के लिए इस चेहरे पर कौन सा आकर्षण है, जिससे बँधी-बँधी वह दिन रात, वर्ष मास अपने को निभाती चली आती है, पर नहीं बुआ के ही घर में होकर यह सोचना मन के शील से परे है...
झिझककर ड्राइंग रूम से निकलता हूँ और अपने कमरे की सीढ़ियाँ चढ़ जाता हूँ। सिगरेट जलाकर झील के दक्खिनी किनारे पर खुलती खिड़की के बाहर देखने लगता हूँ। हरे पहाड़ों के छोटे-बड़े आकारों में टीन की लाल-लाल छतें और बीच-बीच में मटियाली पगडंडियाँ। बुआ खाने तक लौट आएँगी और मन्नो भी तो...देर तक बैठा-बैठा किसी पुराने अखबार के पन्ने पलटता रहा। बुआ लौटी नहीं। घड़ी की टन-टन के साथ नौकर ने खाने के लिए अनुरोध किया।
‘‘खाना लगेगा, साहिब ?’’
‘‘बुआ कब तक लौटेंगी ?’’
‘‘खाने को तो मना कर गई हैं।’’
कथन के रहस्य को मैं इन अर्थहीन सी आँखों में पढ़ जाने के प्रयत्न में रहता हूँ।
‘‘और जो मेहमान हैं ?’’
नौकर तत्परता से झुककर बोला, ‘‘आपके साथ नहीं, साहिब! वह अलग से ऊपर खाएँगी।’’
मैं एक लम्बी साँस भरकर जले सिगरेट के टुकड़े को पैर के नीचे कुचल देता हूँ। शायद साथ खाने के डर से छुटकारा पाने पर या शायद साथ न खा सकने की विवशता पर। उस खाने की मेज पर अकेले खाना खाते-खाते क्या सोचता रहा था, आज तो याद नहीं, बस इतना-सा याद है, काँटे-छुरी से उलझता बार-बार मैं बाहर की ओर देखता था।
मीठा कौर मुँह में लेते ही घोड़े की टाप सुनाई दी, ठिठककर सुना, ‘‘सलाम, साहिब।’’
धीमी मगर सधी आवाज, ‘‘दो घंटे तक पहुँच सकोगे न ?’’
‘‘जी, हुजूर। ’’
सीढ़ियों पर आहट हुई और शायद अपने कमरे तक पहुँचकर खत्म हो गई। खाने के बरतन उठ गए। मैं उठा नहीं। दोबारा कॉफी पी लेने के बाद भी वहीं बैठा रहा। एकाएक मन में आया कि किसी के छोटे से परिचय से मन में इतनी दुविधा उपजा लेना कम छोटी दुर्बलता नहीं है। आखिर किसी से मिल ही लिया हूँ, तो उसके लिए ऐसा-सा क्यों हुआ जा रहा हूँ।
घंटे-भर बाद मैं किसी की पैरों चली सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ा जा रहा था। खुले द्वार पर परदा पड़ा था। हौले से थाप दी।
‘‘चले आइए।’’
परदा उठाकर देहरी पर पाँव रखा। हाथ में कश्मीरी शॉल लिये मन्नो सूटकेस के पास खड़ी थी। देखकर चौंकी नहीं। सहज स्वर में कहा, ‘‘आइए।’’ फिर सोफे पर फैले कपड़े उठाकर कहा, ‘‘बैठिए।’’
बैठते-बैठता सोचा, बुआ के घर भर में सबसे अधिक सजा और साफ कमरा यही है। नया-नया फर्नीचर, कीमती परदे और इन सबमें हल्के पीले कपड़ों में लिपटी मन्नो। अच्छा लगा।
बात करने को कुछ भी न पाकर बोला, ‘‘आप लंच तो...’’
‘‘जी, मैं कर चुकी हूँ।’’ और भरपूर मेरी ओर देखती रही।
मैं जैसे कुछ कहलवा लेने को कहता हूँ, ‘‘बुआ तो कहीं बाहर गई हैं।’’
सिर हिलाकर मन्नो शॉल की तह लगाती है और सूटकेस में रखते-रखते कहती है, ‘‘शाम से पहले ही नीचे उतर जाऊँगी। बुआ से कहिएगा एक ही दिन को आई थी।’’
‘‘बुआ तो आती ही होंगी।’’
इसका उत्तर न शब्दों में आया, न चेहरे पर से। कहते-कहते एक बार रुका, फिर न जाने कैसे आग्रह से कहा, ‘‘एक दिन और नहीं रुक सकेंगी !’’
वह कुछ बोली नहीं। बन्द करते सूटकेस पर झुकी रही।
फिर पल-भर बाद जैसे स्नेह भरे हाथ से अपने बालों को छुआ और हँसकर कहा, ‘‘क्या करूँगी यहाँ रहकर ? भुवाली के इतने बड़े गाँव के बाद यह छोटा सा शहर मन को भाता नहीं।’’
वह छोटी सी खिलखिलाहट, वह कड़वाहट से परे का व्यंग्य, आज इतने वर्षों के बाद भी, मैं वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही सुन रहा हूँ। वही शब्द हैं, वही हँसी और वही पीली-सी सूरत...
हम संग-संग नीचे उतरे थे। मेरी बाँह पर मन्नो का कोट था। नौकर और माली ने झुककर सलाम किया और अतिथि से इनाम पाया। साईस ने घोड़े को थपथपाया।
‘‘हुजूर चढ़ेगी।’’
उड़ती-उड़ती नजर उन आँखों की, बाँह पर लटके कोट पर अटकी।
‘‘पैदल जाऊँगी। घोड़ा आगे-आगे लिए चलो।’’
चाहा कि घोड़े पर चढ़ जाने के लिए अनुरोध करूँ, पर कह नहीं पाया। फाटक से बाहर होते-होते वह पल-भर को पीछे मुड़ी, जैसे छोड़ने के पहले घर को देखती हो। फिर एकाएक अपने को सँभालकर नीचे उतर गई।
टैक्सी खड़ी थी। सामान लदा। ड्राइवर ने उन कठिन क्षणों को मानो भाँपकर कहा, ‘‘कुछ और देर है, साहिब।’’
मन्नो ने इस बार कहीं देखा नहीं। कोट लेने के लिए मेरी ओर हाथ बढ़ा दिया। कार में बैठी तो कुली ने तत्परता से पीछे से कम्बल निकाला और घुटनों पर डालते हुए कहा, ‘‘कुछ, और मेम साहिब ?’’
घुँघराली छाँह ढीली-सी होकर सीट के साथ जा टिकी। घुटनों पर पतली-पतली सी विवश बाँहें फैलाते हुए धीरे से कहा, ‘‘नहीं-नहीं, कुछ और नहीं। धन्यवाद।’’
अधखुले काँच में से अन्दर झाँका। मुख पर थकान के चिह्न थे। बाँहों में मछलीमुखी कंगन थे। आँखों में, क्या था, यह मैं पढ़ नहीं पाया। वही पीली, पतझड़ी दृष्टि उन हाथों पर जमी थी, जो कम्बल पर एक-दूसरे से लगे मौन पड़े थे।
कार स्टार्ट हुई। मैं पीछे हटा और कार चल दी। विदाई के लिए न हाथ उठे, न अधर हिले। मोड़ तक पहुँचने तक पीछे के शीशे से सादगी से बँधा बालों का रिबन देखता रहा और देर तक वह दर्दीले धन्यवाद की गूँज सुनता रहा-नहीं-नहीं, कुछ और नहीं।
वे पल अपनी कल्पना से आज भी लौटता हूँ तो जी को कुछ होने लगता है। उस कार को भगा ले जानेवाली सूखी सड़क से घूमकर मैं ताल के किनारे-किनारे चला जा रहा हूँ। अपने को समझाने-बुझाने पर भी वह चेहरा, वह बीमारी मन पर से नहीं उतरती। रुक-रुककर, थक-थककर जैसे मैं उस दिन घर की चढ़ाई चढ़ा था, उसे याद कर आज भी निढाल हो जाता हूँ। घर पहुँचा। बरामदे में से कुली फर्नीचर निकाल रहे थे। मन धक्का खाकर रह गया। तो उस मन्नो के कमरे की सजावट, सुख-सुविधा सब किराए पर बुआ ने जुटाए थे। दुपहर में बुआ के प्रति जो कुछ जितना भी अच्छा लगा था, वह सब उल्टा हो गया।
आगे बढ़ा, तो द्वार पर बुआ खड़ी थीं। सन्देह से मुझे देख और पास होकर फीके गले से कहा, ‘रवि, मुँह हाथ धो डालो, सामान सब तैयार मिलेगा वहाँ, जल्दी लौटोगे न, चाय लगने को ही है !’’
चुपचाप बाथरूम में पहुँच गया। सामान सब था। मुँह-हाथ धोने से पहले गिलास में ढँककर रखे गर्म पानी से गला साफ किया। ऐसा लगा, किसी की घुटी-घुटी जकड़ में से बाहर निकल आया हूँ। कपड़े बदलकर चाय पर जा बैठा। बच्चे नहीं, केवल बुआ थीं। बुआ ने चाय उँड़ेली और प्याला आगे कर दिया।
‘‘बुआ !’’
बुआ ने जैसे सुना नहीं।
‘‘बुआ, बुआ !’’-पल-भर के लिए अपने को ही कुछ ऐसा सा लगा कि किसी और को पुकारने के लिए बुला को पुकार रहा हूँ। बुआ ने विवश हो आँखें ऊपर उठाईं। समझ गया कि बुआ चाहती हैं, कुछ कहूँ नहीं, पर मैं रुका नहीं।
‘‘बुआ दो दिन की मेहमान तो एक ही दिन में चली गई।’’
सुनकर बुआ चम्मच से अपनी चाय हिलाने लगीं। कुछ बोली नहीं। इस मौन से मैं और भी निर्दयी हो गया।
‘‘कहती थी, बुआ से कहना मैं एक ही दिन को आई थी।’’
इसके आगे बुआ जैसे कुछ और सुन नहीं सकीं। गहरा लम्बा श्वास लेकर आहत आँखों से मुझे देखा, ‘‘तुम कुछ और नहीं कहोगे, रवि....’’ और चाय का प्याला वहीं छोड़ कमरे से बाहर हो गईं।
उस रात दौरे से फूफा के लौटने की बात थी। नौकर से पूछा तो पता लगा, दो दिन के बाद आने का तार आ चुका है। चाहा, एक बार बुआ के कमरे तक हो आऊँ, पर संकोचवश पाँव उठे नहीं। देर बाद सीढ़ियों में अपने को पाया, तो सामने मन्नो का खाली कमरा था। आगे बढ़कर बिजली जलाई, सब खाली था, न परदे, न फर्नीचर...न मन्नो...एकाएक अँगीठी में लगी लकड़ियों को देख मन में आया, आज वह यहाँ रहती, तो रात देर गए इसके पास यहीं बैठी रहती और मैं शायद इसी तरह जैसे अब यहाँ आया हूँ, उसके पास आता, उसके...
यह सब मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ...
किसी अनदेखे भय से घबराकर नीचे उतर आया। खिड़की से बाहर देखा, अँधेरा था। सिरहाना खींचा, बिजली बुझाई और बिस्तर पर पड़े-पड़े भुवाली की वह छोटी सी कॉटेज देखता रहा, जहाँ अब तक मन्नो पहुँच गई होगी।
‘‘रवि !’’
मैं चौंका नहीं, यह बुआ का स्वर था। बुआ अँधेरे में ही पास आ बैठीं और हौले-हौले सिर सहलाती रहीं।
‘‘बुआ।’’
बुआ का हाथ पल-भर को थमा फिर कुछ झुककर मेरे माथे तक आ गया। रुँधे स्वर से कहा, ‘‘रवि, तुम्हें नहीं, उस लड़की को दुलराती हूँ। अब यह हाथ उस तक नहीं पहुँचता...’’
मैं बुआ का नहीं, मन्नो का हाथ पकड़ लेता हूँ।
बुआ देर तक कुछ नहीं बोलीं। फिर जैसे कुछ समझते हुए अपने को कड़ा कर कहा, ‘‘रवि, उसके लिए कुछ मत सोचो, उसे अब रहना नहीं है।’’
मैं बुआ के स्पर्श तले सिहरकर कहता हूँ, ‘‘बुआ, मुझे ही कौन रहना है ?’’
आज वर्षों बाद भुवाली में पड़े-पड़े मैं असंख्य बार सोचता हूँ कि उस रात मैं अपने लिए यह क्यों कह गया था ! क्यों कह गया था वे अभिशाप के बोल, जो दिन-रात मेरे इस तन-मन पर से सच्चे उतरे जा रहे हैं ? सुनकर बुआ को कैसा लगा, नहीं जानता। वे हाथ खींचकर उठीं। रोशनी की, और पूरी आँखों से मुझे देखकर अविश्वास और भर्त्सना से कहा, ‘‘पागल हो गए हो, रवि ! उसके साथ अपनी बात जोड़ते हो, जिसके लिए कोई राह नहीं रह गई, कोई और राह नहीं रह गई।’’
फिर कुर्सी पर बैठते-बैठते कहा, ‘‘रवि, तुम तो उसे सुबह-शाम तक ही देख पाए हो। मैं वर्षों से उसे देखती आई हूँ और आज पत्थर-सी निष्ठुर हो गई हूँ। उसे अपना बच्चा ही करके मानती रही हूँ, यह नहीं कहूँगी। अपने बच्चों की तरह तो अपने बच्चों के सिवाय और किस रखा जा सकता है ! पर जो कुछ जितना भी था, वह प्यार वह देखभाल सब व्यर्थ हो गए हैं। कभी छुट्टी के दिन उसका बोर्डिग से आने की राह तकती थी, अब उसके आने से पहले उसके जाने का क्षण मनाती हूँ और डरकर बच्चों को लिये घर से बाहर निकल जाती हूँ।’’
बुआ के बोल कठिन हो आए।
‘‘रवि, जिसे बचपन में मोहवश कभी डराना नहीं चाहती थी, आज उसी से डरने लगी हूँ। उसकी बीमारी से डरने लगी हूँ।’’ फिर स्वर बदलकर कहा, ‘‘तुम्हारा ऐसा जीवट मुझमें नहीं कि कहूँ, डरती हूँ।’’ बुआ ने यह कहकर जैसे मुझे टटोला-और मैं बिना हिलेडुले चुपचाप लेटा रहा।
बुआ असमंजस में देर तक मुझे देखती रहीं। फिर जाने को उठीं और और रुक गईं। इस बार स्वर में आग्रह नहीं, चेतावनी थी, ‘‘रवि, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जिसके लिए सब राह रुकी हों, उसके लिए भटको नहीं।’’
पर उस दिन बुआ की बात मैं समझा नहीं, चाहने पर भी नहीं।
अगली सुबह चाहा कि घूम-घूमकर दिन बिता दूँ। घोड़ा दौड़ाता लड़ियाकाँटा पहुँचा और उन्हीं पैरों लौट आया। घर की ओर मुँह करते करते, न जाने क्यों, मन को कुछ ऐसा लगा कि मुझे घर नहीं, कहीं और पहुँचना है। चढ़ाई के मोड़ पर कुछ देर खड़ा-खड़ा सोचता रहा और जब ढलती दुपहरी में तल्लीताल की उतराई उतरा तो मन के आगे सब साफ था।
मुझे भुवाली जाना था।
बस से उतरा। अड्डे पर रामगढ़ के लाल-लाल सेबों के ढेर देखकर यह नहीं लगा कि यही भुवाली है। बस में सोचता आया था कि वहाँ घुटन होगी; पर चीड़ के ऊँचे-ऊँचे पेड़ों से लहराती हवाएँ बह-बह आती थीं। छाँह ऊपर उठती है, धूप नीचे उतरती है और भुवाली मन को अच्छी लगती है। तन को अच्छी लगती है। चौराहे से होकर पोस्ट-ऑफिस पहुँचा। कॉटेज का पता लगा लिया और छोटे से पहाड़ी बाजार में होता हुआ ‘पाइंस’ की ओर हो लिया। खुली-चौड़ी सड़क के मोड़ से अच्छी सी पतली राह ऊपर जा रही थी। जँगले से नीचे देखा, अलग-अलग खड़े पहाड़ों के बीच की जगह पर एक खुली-चौड़ी घाटी बिछी थी। तिरछे-सीछे, खेत किसी के घुटने पर रखे कसीदे के कपड़े की तरह धरती पर फैले थे। दूर सामने दक्खिन की ओर पानी का ताल धूप में चाँदी के थाल की तरह चमकता था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book