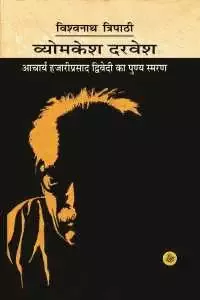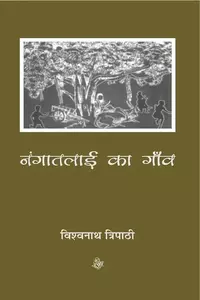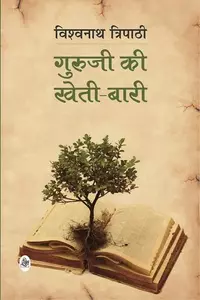|
लेख-निबंध >> देश के इस दौर में देश के इस दौर मेंविश्वनाथ त्रिपाठी
|
37 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है परसाई के व्यंग्य-निबंधों की विवेचना.....
Desh Ke Is Daur Main Vishvanath Tripathi
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
परसाई जी पर आपकी किताब मिल गई और पढ़ ली गई। अपने देश व समाज से, मानवता से आप जिस गहराई तक जुड़े हैं, उस पर अचम्भा होता है। बहुत-सी चीजें साफ होती हैं। परसाई जी का मैं प्रशंसक हूँ, आज से नहीं, बहुत पहले से। हिन्दी मे आज तक ऐसा हास्य-व्यंग्यकार नहीं हुआ। आपने बहुत बड़ा काम किया है। परसाई जी की जीवन कृतित्व दोनों को मिलाकर एक पुस्तक लिखी जानी चाहिए।
अमरकान्त
परसाई पर विश्वनाथ त्रिपाठी ने पहली बार गम्भीरता से विचार किया है। यह अभी तक की एक अनुपम और अद्वितीय पुस्तक है, जिसमें परसाई के रचना-संसार को समझने और उदघाटित करने का प्रयास किया है।
ज्ञानरंजन
परसाई का लेखन डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी के चिन्तन के करीब पड़ता है। वे चिन्तन को परसाई की रचना से पुष्ट और समृद्ध करते हैं। परसाई जी के निबन्घों की उन्होंने बहुत तरह से, बहुत कोणों से जाँच-पड़ताल की है-वर्तमान की दृष्टि से, मनोविकारों की दृष्टि से, कला की दृष्टि से और रूप की दृष्टि से।
वर्तमान की पहचान समझ और संवेदना
परसाई वर्तमान के रचनाकार हैं। इस कथन का मतलब केवल यह नहीं है कि उनके लेखन में आजादी के बाद की स्थितियों का चित्रण है। वर्तमानता उनकी रचनाधर्मिता के केन्द्र में है, वह रचनात्मक मूल्य बन गयी है। परसाई के शब्दों में:-
‘‘शाश्वत लिखने वाले तुरन्त मुत्यु को प्राप्त होते हैं। अपना लिखा जो रोज़ मरता देखते हैं वही अमर होते हैं वही अमर होते हैं-जो अपने युग के प्रति ईमानदार नहीं है वह अनंतकाल के प्रति क्या ईमानदार होगा।’’
शाश्वत अरूप है, सरूप-और सबसे ज्यादा सरूप वर्तमान है। लेखक सरूप वर्तमान से प्रभावित न हो, और जिसे नहीं देख रहा, उसी से प्रभावित होने का प्रयास करे या ढोंग रचे तो वह अपनी समझ में शाश्वत लिखेगा। विभिन्न युगों के ‘वर्तमानों’ के योग के आधार पर हम शाश्वत की कल्पना करते हैं। इसी को निराला कहते थे-हम नित्य नवीनता में ही सनातनता पाते हैं।
काल को भूत, भविष्य, वर्तमान में बाँट दिया गया है, समझने-समझने की सुविधा के लिए भूत और भविष्य को वर्तमान जोड़ता और काटता है। भूत वर्तमान में प्रतिफलित होता है-वर्तमान में भूत निहित है। वर्तमान की सक्रियता भविष्य का निर्माण करती है। वर्तमान का सर्वाधिक महत्त्व इस बात में है कि वह सक्रियता से जुड़ा है। हम वर्तमान में ही कार्यरत होते हैं। अतीत, में हम नहीं हमारे पूर्वज कार्यरत थे। भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ उद्योग करेंगी। भविष्य में काम करने की हम योजना ही बना सकते हैं। काल को कर्म में हम केवल वर्तमान में ढाल सकते हैं। यह बात मुक्तबोध की एक पंक्ति- ‘पीतालोक प्रसार के काल गल रहा है’ से स्पष्ट होती है। ‘अँधेरे में’ कविता का वाचक निष्क्रिय है। इसलिए काल गल रहा है। पीत आलोक निष्क्रियता का घोतक है। रक्त आलोक सकर्मकता का।
हरिशंकर परसाई वर्तमानता के रचनाकार हैं। उनका साहित्य बीसवीं सदी के उत्तरार्ध के भारत का है। यह साहित्य इस काल के साहित्य की पहचान है। परसाई ने वर्तमान समस्याओं को ही अपने लेखन का आधार बनाया है। आधुनिक काल के किसी अन्य रचनाकार ने वर्तमान समस्याओं तक ही अपने को इतना व्यक्त नहीं रखा है। वर्तमान समस्याओं को लिखते समय रचनाकार उन्हीं समस्याओं पर कलम चलाते हैं जिस पर लोगों का ध्यान केंद्रित हो चुका है। ये सीमित वर्तमान के रचनाकार हैं। वर्तमान के मामूलीपन या ‘रोजमर्रा’ को रचना में इतना प्रतिष्ठित पहले, किसी और ने नहीं किया था। यह प्रगतिशीलता का विकास है। जीवन की सामान्य बातों को रचना में स्थान देकर भारतेंदु ने हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तन किया था। वह आधुनिकता प्रगतिशीलता भी थी। बालमुकुंद गुप्त द्वारा लिखित शिवशंभु के चिट्ठे में हम इसी मामूलीपन की प्रतिष्ठा पाते हैं। किंतु स्वातंत्र्योत्तर भारत की विशिष्ट स्थितियों में इस रोजमर्रा मामूलीपन के महत्त्व में गुणात्मक परिवर्तन हो गया है। हिंदी में यह मामूलीपन कविता में नागार्जुन और गद्य में हरिशंकर परसाई के यहाँ सबसे ज्यादा दिखलाई पड़ा है। कविता में सामान्य स्थितियों को आधार बनाकर रचना करने की दीर्घ परंपरा लोक साहित्य में रही है, नागार्जुन ने उसका काफी सहारा लिया। परसाई के पूर्वज इस दृष्टि से केवल बालमुकुंद गुप्त हैं। उनका गद्य विधा की दृष्टि से अत्यंत प्रयोगपूर्ण और नवीन है। वह बालमुकुंद गुप्त के ‘शिवशंभु के चिट्ठे’ से भी भिन्न है। हरिशंकर परसाई के निबंधों में भंग की तरंग की भूमिका नहीं। वे छदम को उद्घाटित कर देने वाली समझ के साथ रचना में प्रवृत्त होते हैं। मदहोश होकर होश की बातें करने के लिए भँगेड़ी की भूमिका में उतरते थे। जबकि परसाई की रचना में सतर्क बोध आद्यंत साथ रहता है।
स्वातंत्र्योत्तर भारत की स्थिति जितनी ज़टिल, छदमपूर्ण है, परसाई की दृष्टि भी उतनी ही काइयाँ और भेदक। यहाँ ईमानदारी तो है किंतु वह मध्यकालीन वीरोचित तेवर से रहित है। परसाई की ईमानदारी आदर्श से प्रेरित है किंतु आदर्शवादी नहीं। वह भी जटिल, काइयाँ, छदम को भेदने में सक्रिय और नाटकीय है। व्यंग्यकार परसाई की नैतिकता मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है किंतु उसकी रणनीति नई है। वह अनैतिक शक्तियों के दांवपेंच से परिचित और उन्हें मात देने में माहिर और शातिर है। उन्हें पढ़ते हुए ब्रेख़्त की याद आती है।
परसाई की रचना को आज़ादी के बाद की स्थितियों से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। आज़ादी के बाद की स्थितियाँ जैसी घटित हुईं वैसी न होतीं तो परसाई का लेखन भी वैसा न होता जैसा कि है। यह बात कमोवेश तो स्वातंत्र्योत्तर भारत के सभी प्रसिद्ध रचनाकारों के बारे में कही जा सकती है, किंतु सबसे ज्यादा यह लागू होती है परसाई के बारे में। साहित्येतर स्थितियाँ रचनात्मक अनिवार्यता निर्मित करती हैं। महान् साहित्य अनिवार्य होता है। परसाई के लेखन में रोजमर्रा का मामूलीपन अनिवार्य भी बन गया है। उनके प्रचुर और पर्याप्त लेखन का आधार अति-सामान्य, परिचित, वर्तमानकालिक, प्रत्यक्ष जीवन जगत् है लेकिन उसका कोई अंश फालतू या महत्त्वहीन नहीं। भाव-परिधि का यह विस्तार अभिभूतकारी और आश्चर्य जनक है पढ़ते समय वे जितना सजग लगते हैं विचार करने पर उतना ही जटिल।
परसाई के निबंधों का आकार बहुत छोटा है। प्रायः दो-तीन पृष्ठों का उन्हें अलग-अगल पढ़ने पर कौतूहल, हास्य, व्यंग्य, घृणा, आक्रोश सब होता है। लेकिन निबंध पढ़ने पर एक झटका जरूर लगता है। कुछ ऐसा हो रहा है जो विक्षुब्ध कर जाता है। विक्षुब्ध करने का गुण ही परसाई को रचनाकार बनाता है-गंभीर रचनाकार। गंभीर रचनाकार मानवतावादी होगा, उसकी रचना का प्रधान तत्त्व करुणा होगा। लेकिन इन निबंधों को आप एक साथ पढ़ें तो ये परस्पर-संबद्ध लगेंगे। पूरा निबंध-साहित्य एक वृहत् युग-गाथा है। व्यंग्य निबंधों का यह महाकाव्यात्मक प्रभाव हिंदी की नई उपलब्धि है। वर्तमानता, मामूलीपन, की अनिवार्यता, महत्ता इन सबके साथ परसाई के निबंधों के शिल्प और विधा के नएपन का अन्योन्यासित सम्बन्ध है।
स्वातंत्र्योत्तर भारत का यथार्थ-बनता बिग़ड़ता हुआ सक्रिय यथार्थ परसाई के निबंधों में विचित्र है। इस सक्रियता, विकासमानता को रेखांकित करने के लिए ही उसके वास्ते ‘वर्तमानता’ शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। यथार्थ असीम है। लेखन-विषय के रूप में वर्तमानता कभी चुकेगी नहीं। वर्तमानता निरंतर विकासनशील है। वर्तमान अपनी अंतस्संबंधता में पहचाना जाता है। हमारे वर्तमान में कितनी समस्याएँ हैं, इन समस्याओं की कितनी पर्तें हैं ! उनके ऐतिहासिक आर्थिक, सांस्कृतिक कारण और दबाव हैं ? विभिन्न वर्गों और वर्गों ही नहीं, एक-एक व्यक्ति पर इन सब का अलग-अलग, समान और असामान्य प्रभाव है। असंख्य व्यक्तियों द्वारा साक्षात अनुभूत किया जाता है। अखंड यानी परस्परसंबंधित है। मार्क्स ने कहा था-प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु से जुड़ी है। वर्तमानता की अखंडता कोई अरूप अलौकिक तत्त्व नहीं। वह हमारे सामने है, हम पर चोट करती हुई, हमें क्षत-विक्षत, आहत, मुदित, पुलकित करती हुई- हमें ललकारती हुई। हमारे हमारे साथ देशवासी झेल रहे हैं। संस्कृति, अतीत-गौरव, पुराण-गाथा, मिथक सब वर्तमान पर घटित हो रहे हैं। वर्तमान का चक्र उन्हें काट-छाँट, खराद रहा है। क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से खुद वर्तमान भी बन रहा है और मिटता हुआ भविष्य में ढल भी रहा है। इन मूल्यों की कसौटी यह है कि समाज और व्यक्ति के ऐतिहासिक वर्तमान में वे कितने सहायक या बाधक हैं। सत्ता, समाज, और व्यक्ति की घोषणाएँ वस्तुतः क्या हैं ? कथनी की करनी क्या है ?
हमारे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारतीय महाकाव्यों के आदर्श उदात्त नायक हैं। महाकवि तुलसीदास ने वर्षा ऋतु में उनके विरह का वर्णन किया। राम ने वर्षा ऋतु में बादलों का गर्जन सुनकर कहा-
‘‘शाश्वत लिखने वाले तुरन्त मुत्यु को प्राप्त होते हैं। अपना लिखा जो रोज़ मरता देखते हैं वही अमर होते हैं वही अमर होते हैं-जो अपने युग के प्रति ईमानदार नहीं है वह अनंतकाल के प्रति क्या ईमानदार होगा।’’
शाश्वत अरूप है, सरूप-और सबसे ज्यादा सरूप वर्तमान है। लेखक सरूप वर्तमान से प्रभावित न हो, और जिसे नहीं देख रहा, उसी से प्रभावित होने का प्रयास करे या ढोंग रचे तो वह अपनी समझ में शाश्वत लिखेगा। विभिन्न युगों के ‘वर्तमानों’ के योग के आधार पर हम शाश्वत की कल्पना करते हैं। इसी को निराला कहते थे-हम नित्य नवीनता में ही सनातनता पाते हैं।
काल को भूत, भविष्य, वर्तमान में बाँट दिया गया है, समझने-समझने की सुविधा के लिए भूत और भविष्य को वर्तमान जोड़ता और काटता है। भूत वर्तमान में प्रतिफलित होता है-वर्तमान में भूत निहित है। वर्तमान की सक्रियता भविष्य का निर्माण करती है। वर्तमान का सर्वाधिक महत्त्व इस बात में है कि वह सक्रियता से जुड़ा है। हम वर्तमान में ही कार्यरत होते हैं। अतीत, में हम नहीं हमारे पूर्वज कार्यरत थे। भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ उद्योग करेंगी। भविष्य में काम करने की हम योजना ही बना सकते हैं। काल को कर्म में हम केवल वर्तमान में ढाल सकते हैं। यह बात मुक्तबोध की एक पंक्ति- ‘पीतालोक प्रसार के काल गल रहा है’ से स्पष्ट होती है। ‘अँधेरे में’ कविता का वाचक निष्क्रिय है। इसलिए काल गल रहा है। पीत आलोक निष्क्रियता का घोतक है। रक्त आलोक सकर्मकता का।
हरिशंकर परसाई वर्तमानता के रचनाकार हैं। उनका साहित्य बीसवीं सदी के उत्तरार्ध के भारत का है। यह साहित्य इस काल के साहित्य की पहचान है। परसाई ने वर्तमान समस्याओं को ही अपने लेखन का आधार बनाया है। आधुनिक काल के किसी अन्य रचनाकार ने वर्तमान समस्याओं तक ही अपने को इतना व्यक्त नहीं रखा है। वर्तमान समस्याओं को लिखते समय रचनाकार उन्हीं समस्याओं पर कलम चलाते हैं जिस पर लोगों का ध्यान केंद्रित हो चुका है। ये सीमित वर्तमान के रचनाकार हैं। वर्तमान के मामूलीपन या ‘रोजमर्रा’ को रचना में इतना प्रतिष्ठित पहले, किसी और ने नहीं किया था। यह प्रगतिशीलता का विकास है। जीवन की सामान्य बातों को रचना में स्थान देकर भारतेंदु ने हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तन किया था। वह आधुनिकता प्रगतिशीलता भी थी। बालमुकुंद गुप्त द्वारा लिखित शिवशंभु के चिट्ठे में हम इसी मामूलीपन की प्रतिष्ठा पाते हैं। किंतु स्वातंत्र्योत्तर भारत की विशिष्ट स्थितियों में इस रोजमर्रा मामूलीपन के महत्त्व में गुणात्मक परिवर्तन हो गया है। हिंदी में यह मामूलीपन कविता में नागार्जुन और गद्य में हरिशंकर परसाई के यहाँ सबसे ज्यादा दिखलाई पड़ा है। कविता में सामान्य स्थितियों को आधार बनाकर रचना करने की दीर्घ परंपरा लोक साहित्य में रही है, नागार्जुन ने उसका काफी सहारा लिया। परसाई के पूर्वज इस दृष्टि से केवल बालमुकुंद गुप्त हैं। उनका गद्य विधा की दृष्टि से अत्यंत प्रयोगपूर्ण और नवीन है। वह बालमुकुंद गुप्त के ‘शिवशंभु के चिट्ठे’ से भी भिन्न है। हरिशंकर परसाई के निबंधों में भंग की तरंग की भूमिका नहीं। वे छदम को उद्घाटित कर देने वाली समझ के साथ रचना में प्रवृत्त होते हैं। मदहोश होकर होश की बातें करने के लिए भँगेड़ी की भूमिका में उतरते थे। जबकि परसाई की रचना में सतर्क बोध आद्यंत साथ रहता है।
स्वातंत्र्योत्तर भारत की स्थिति जितनी ज़टिल, छदमपूर्ण है, परसाई की दृष्टि भी उतनी ही काइयाँ और भेदक। यहाँ ईमानदारी तो है किंतु वह मध्यकालीन वीरोचित तेवर से रहित है। परसाई की ईमानदारी आदर्श से प्रेरित है किंतु आदर्शवादी नहीं। वह भी जटिल, काइयाँ, छदम को भेदने में सक्रिय और नाटकीय है। व्यंग्यकार परसाई की नैतिकता मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है किंतु उसकी रणनीति नई है। वह अनैतिक शक्तियों के दांवपेंच से परिचित और उन्हें मात देने में माहिर और शातिर है। उन्हें पढ़ते हुए ब्रेख़्त की याद आती है।
परसाई की रचना को आज़ादी के बाद की स्थितियों से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। आज़ादी के बाद की स्थितियाँ जैसी घटित हुईं वैसी न होतीं तो परसाई का लेखन भी वैसा न होता जैसा कि है। यह बात कमोवेश तो स्वातंत्र्योत्तर भारत के सभी प्रसिद्ध रचनाकारों के बारे में कही जा सकती है, किंतु सबसे ज्यादा यह लागू होती है परसाई के बारे में। साहित्येतर स्थितियाँ रचनात्मक अनिवार्यता निर्मित करती हैं। महान् साहित्य अनिवार्य होता है। परसाई के लेखन में रोजमर्रा का मामूलीपन अनिवार्य भी बन गया है। उनके प्रचुर और पर्याप्त लेखन का आधार अति-सामान्य, परिचित, वर्तमानकालिक, प्रत्यक्ष जीवन जगत् है लेकिन उसका कोई अंश फालतू या महत्त्वहीन नहीं। भाव-परिधि का यह विस्तार अभिभूतकारी और आश्चर्य जनक है पढ़ते समय वे जितना सजग लगते हैं विचार करने पर उतना ही जटिल।
परसाई के निबंधों का आकार बहुत छोटा है। प्रायः दो-तीन पृष्ठों का उन्हें अलग-अगल पढ़ने पर कौतूहल, हास्य, व्यंग्य, घृणा, आक्रोश सब होता है। लेकिन निबंध पढ़ने पर एक झटका जरूर लगता है। कुछ ऐसा हो रहा है जो विक्षुब्ध कर जाता है। विक्षुब्ध करने का गुण ही परसाई को रचनाकार बनाता है-गंभीर रचनाकार। गंभीर रचनाकार मानवतावादी होगा, उसकी रचना का प्रधान तत्त्व करुणा होगा। लेकिन इन निबंधों को आप एक साथ पढ़ें तो ये परस्पर-संबद्ध लगेंगे। पूरा निबंध-साहित्य एक वृहत् युग-गाथा है। व्यंग्य निबंधों का यह महाकाव्यात्मक प्रभाव हिंदी की नई उपलब्धि है। वर्तमानता, मामूलीपन, की अनिवार्यता, महत्ता इन सबके साथ परसाई के निबंधों के शिल्प और विधा के नएपन का अन्योन्यासित सम्बन्ध है।
स्वातंत्र्योत्तर भारत का यथार्थ-बनता बिग़ड़ता हुआ सक्रिय यथार्थ परसाई के निबंधों में विचित्र है। इस सक्रियता, विकासमानता को रेखांकित करने के लिए ही उसके वास्ते ‘वर्तमानता’ शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। यथार्थ असीम है। लेखन-विषय के रूप में वर्तमानता कभी चुकेगी नहीं। वर्तमानता निरंतर विकासनशील है। वर्तमान अपनी अंतस्संबंधता में पहचाना जाता है। हमारे वर्तमान में कितनी समस्याएँ हैं, इन समस्याओं की कितनी पर्तें हैं ! उनके ऐतिहासिक आर्थिक, सांस्कृतिक कारण और दबाव हैं ? विभिन्न वर्गों और वर्गों ही नहीं, एक-एक व्यक्ति पर इन सब का अलग-अलग, समान और असामान्य प्रभाव है। असंख्य व्यक्तियों द्वारा साक्षात अनुभूत किया जाता है। अखंड यानी परस्परसंबंधित है। मार्क्स ने कहा था-प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु से जुड़ी है। वर्तमानता की अखंडता कोई अरूप अलौकिक तत्त्व नहीं। वह हमारे सामने है, हम पर चोट करती हुई, हमें क्षत-विक्षत, आहत, मुदित, पुलकित करती हुई- हमें ललकारती हुई। हमारे हमारे साथ देशवासी झेल रहे हैं। संस्कृति, अतीत-गौरव, पुराण-गाथा, मिथक सब वर्तमान पर घटित हो रहे हैं। वर्तमान का चक्र उन्हें काट-छाँट, खराद रहा है। क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से खुद वर्तमान भी बन रहा है और मिटता हुआ भविष्य में ढल भी रहा है। इन मूल्यों की कसौटी यह है कि समाज और व्यक्ति के ऐतिहासिक वर्तमान में वे कितने सहायक या बाधक हैं। सत्ता, समाज, और व्यक्ति की घोषणाएँ वस्तुतः क्या हैं ? कथनी की करनी क्या है ?
हमारे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारतीय महाकाव्यों के आदर्श उदात्त नायक हैं। महाकवि तुलसीदास ने वर्षा ऋतु में उनके विरह का वर्णन किया। राम ने वर्षा ऋतु में बादलों का गर्जन सुनकर कहा-
घन घमंड गरजत घन घोर।
प्रियाहीन डरपत मन मोर।।
प्रियाहीन डरपत मन मोर।।
यह पंक्ति लोगों की ज़बान पर है लेकिन इस पंक्ति को पढ़ने वाले की छत टपक रही है। उसे तुलसीदास के राम की स्थिति में आने की सुविधा नहीं वह राम की नहीं ग़ालिब की स्थिति में है।
गालिब का मकान भी मेरे जैसा होगा। तभी एक चिट्ठी में लिखा है आस्माँ एक घंटा बरसे तो घर दिन भर।’ इसमें राम को मिथक की दुनिया से निकालकर अपनी स्थिति में डाल दिया गया है। तब क्या हुआ ?
‘राम की बात राम जानें। बादलों की गर्जन से डरता मैं भी हूँ, पर इस डर का कारण जानता हूँ। नहीं, राम वाला कारण नहीं है। मेरे डर का कारण कोई हरण की गई प्रिया नहीं है, यह मकान है, जिसकी छाया तले बैठा हूँ। राम इस भय को नहीं जानते थे। वे किसी किराए के मकान में चतुर्मास काटते तो भाई को ऐसी बातें थोड़े ही सिखाते कि हे लक्ष्मण, पर्वत बूंदों के आघात को ऐसे सह रहे हैं, जैसे संत-जन दुष्टों के वचन सहते हैं। वे कहते हैं कि हे लक्ष्मण ! मेरे ठीक सिरहाने एक बड़ा टपका है, मुझे रात को नींद नहीं आई। आज ठीक कराना। और लक्ष्मण ‘जो आज्ञा’ कहकर मकान वाले से शिकायत करने चल देते। पर्वत चाहे बूंदों का आघात कितना ही सहें, लक्ष्मण बर्दाश्त नहीं करते। वे बाण मारकर बादलों को भगा देते या मकान-मालिक का ही शिरच्छेद कर देते।’ (3/16) 1
इसमें राम को उनकी मिथकीय दुनियां से निकालकर टपकने वाली छत के नीचे रहने वाले निम्नमध्यवर्गीय किराएदार के साथ कर दिया गया है। पुराण-गाथा या रोमांचक साहित्य हमें अपनी स्थिति से ऊपर उड़ा ले जाता है। यहाँ निम्नमध्यवर्गीय व्यक्ति की स्थिति पुराण, गाथा, मिथक को अपनी तरह बना लेती है। अपनी स्थिति का अविस्मरणीय आग्रह परसाई के व्यंग्य निबंधों की विशेषता है, वे मिथकों का उपयोग मिथक-भंजन के लिए करते हैं। इससे वर्तमान या वस्तुस्थिति उजागर होती है।
हम जानते हैं कि पौराणिक नायकों को वर्तमान में पहले भी लाया गया है, अब भी लाया जाता हैः ‘मानुस हौं तो बही कवि चोंच बसौं नित टेम्स नदी के किनारे/ ’जो पशु हौं तो बनौं बुलडाग चलौं नितकार में पूँछ निकारे/’ आदि में भी यही किया गया है। पौराणिक पात्रों को आधुनिक स्थितियों में डालकर, नए फैशन की हँसी उड़ाना हिंदी व्यंग्य में बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। लेकिन ऐसे लोग वर्तमानता को परसाई की तरह नहीं देखते। परसाई की दृष्टि द्वंद्वात्मक है। उनके यहाँ वर्तमानता एक ऐतिहासिक अवधारणा और मूल्य है। वे पौराणिक पात्रों की टक्कर प्रायः निम्नमध्यवर्गीय, अभावग्रस्त या शोभित पात्रों से कराते हैं। उनके यहाँ ये पौराणिक पात्र वर्तमान युग की जटिल विषमता में उलझकर अपनी पौराणिक गरिमा झाड़ देते हैं। अभावग्रस्त शोभित जन के प्रति बेहद करुणा ही परसाई को कबीर और गा़लिब से जोड़ती है। यह करुणा व्यंग्य में छिपी रहती है। परसाई को कबीर और गालिब से जोड़ती है। यह करुणा व्यंग्य में छिपी रहती है।
परसाई को कबीर और ग़ालिब से यों ही नहीं जोड़ा
1. (3/16) परसाई रचनावली, खंड 3, पृष्ठ 16 का सूचक है। आगे भी यही क्रम है।
परसाई को कबीर और ग़ालिब से यों ही नहीं जोड़ा जा रहा है। इस पर यथावसर चर्चा की जाएगी।
परसाई के लेखन को समग्रता में देखा जाए तो वर्तमान भारत के द्वंद्व का चित्र उभरेगा। इस चित्र में एक कसमसाता, छटपटाता हुआ भारत है जिसे एक और छद्म भारत ने दबोच रखा है। दबोचने वाला और दमित दोनों भारत सक्रिय हैं। दोनों के बीच निरंतर दाव-पेंच चल रहे हैं। शोषक-शोषित उनकी समस्याएँ, सांस्कृतिक, आर्थिक आचरण सब परम्पर संबद्ध हैं। इस सघन परम्परा-संबंधता को ही वर्तमानता की अखंडता समझिए। इससे उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग सब की आशाएँ, आकांक्षाएँ हैं। सबके अपने-अपने दुःख हैं। दुख और सुख विविध हैं, भिन्न हैं, परस्पर विरोधी हैं, छद्म हैं, सच्चे हैं।
‘मेरा दुख यह है कि मुझे बिजली का 40 रू. का बिल जमा करना है और मेरे पास इतने रुपए नहीं है।
तभी एक बंधु अपना दुख बताने लगता है। उसने 8 कमरों का मकान बनाने की योजना बनाई थी।6 कमरे बन चुके हैं। 2 के लिए पैसे की तंगी आ गयी है।
एक बंधु की रोटरी मशीन आ गयी है। अब मोनो मशीन आने में कठिनाई आ गई है। वे दुखी हैं।
एक जीवित रहने का संघर्ष है और एक संपन्नता का संघर्ष।’ (3/ 45-46)
सतर्क वैज्ञानिक-बोध परसाई की रचना का प्रधान साधक है। वे इस बोध से संस्थानों, रूढ़ियों, आचरण आदि के टुकड़े कर देते हैं और उनका व्यंग्य वास्तविकता प्रकट कर देता है। चूँकि अमानवीय है अतएव इसकी अनुभूति करुणा जगाती है।
स्वातंत्र्योत्तर भारत स्वाधीनता आंदोलन के सिद्धांत गायब नहीं हो गए हैं। उनका इस्तेमाल किया जाता है मुखौटों के रूप में। कथनी और करनी में भिन्नता नहीं, विपरीतता है। फलतः देश में मानवीय विरासत को मुखौटै के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह हमारे देश में ज्यादा आसान है क्योंकि हमारे देश की जनता का अधिकांश रूढ़िग्रस्त है। जो शिक्षित हैं उनकी आँखों पर भी रूढ़ि और अंधविश्वास का आवरण पड़ा है। जनता का शोषण करने वाली शक्तियाँ एक हो जाती हैं। सांप्रदायिकता, बहुराष्ट्रीय पूँजी, फासिज्म, धर्म, वर्ग-विभाजन को बरकरार रखने वाली राजनीतिक शक्तियाँ सब इस नाटकीय षड्यंत्र में शामिल होकर एक जुट हो जाती हैं।
राजनीतिज्ञ स्वाधीनता आंदोलन के नारों-सत्य, अहिंसा, सेवा को, धर्माधिकारी अतीत को, फासिज्म संस्कृति को मुखौटा बनाते हैं तो देशी पूँजीवाद और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ सब कुछ इस्तेमाल विज्ञापन के रूप में करती हैं। विज्ञापन हमारे युग का सबसे बड़ा और घातक मुख़ौटा है। वह आर्थिक शोषण के लिए राजनैतिक, चरित्र, संस्कृति, मानसिकता को विकृत करता है। नारी को शारीरिकता में सीमित करता है। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि पूँजीवाद सामंती दृष्टि का ही विकास है। इसके लिए क्षणवाद एवं व्यक्तिवादी अनुभववाद सहायक होते हैं।
परसाई यह सारा छद्म देख लेते हैं तो इसका श्रेय उस वैज्ञानिक दृष्टि को भी है जो पूँजीवादी के विरोध में समाजवादी विकास का विकल्प प्रस्तुत करती है। साम्राज्यवाद से समर्पित, कभी-कभी उससे अपने स्वार्थ के लिए टकराता हुआ भी, देशी पूँजीवीद और अनेकता के साथ एकता में विश्वास करने वाला समाजवाद-इन दोनों का परस्पर विरोध हमारे युग की वर्तमानता का अंतर्विरोधी है। इसे हमारे देश का प्रत्येक जन झेल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति इस संघर्ष-गाथा का पात्र है। हम जब आँकड़ों का सिद्धांतों की भाषा में बहस करते हैं, तब इस संघर्ष गाथा की अनुभव धार बहुत कुछ अरूप होकर ओझल हो जाती है। देश के एक-एक जन का दुःख अनुभव अपने आप में अखंड है। इन सबके अनुभवों को एक साथ देखने का प्रयास करने वाला रचनाकार अपने युग का महाकाव्य लिखता है। इस व्याप्ति में प्रत्येक का संघर्ष ओझल नहीं होता। यही वर्तमानता है। मुक्तिबोध पीड़ा में जो व्याप्ति है, वह दृष्टव्य हैः
गालिब का मकान भी मेरे जैसा होगा। तभी एक चिट्ठी में लिखा है आस्माँ एक घंटा बरसे तो घर दिन भर।’ इसमें राम को मिथक की दुनिया से निकालकर अपनी स्थिति में डाल दिया गया है। तब क्या हुआ ?
‘राम की बात राम जानें। बादलों की गर्जन से डरता मैं भी हूँ, पर इस डर का कारण जानता हूँ। नहीं, राम वाला कारण नहीं है। मेरे डर का कारण कोई हरण की गई प्रिया नहीं है, यह मकान है, जिसकी छाया तले बैठा हूँ। राम इस भय को नहीं जानते थे। वे किसी किराए के मकान में चतुर्मास काटते तो भाई को ऐसी बातें थोड़े ही सिखाते कि हे लक्ष्मण, पर्वत बूंदों के आघात को ऐसे सह रहे हैं, जैसे संत-जन दुष्टों के वचन सहते हैं। वे कहते हैं कि हे लक्ष्मण ! मेरे ठीक सिरहाने एक बड़ा टपका है, मुझे रात को नींद नहीं आई। आज ठीक कराना। और लक्ष्मण ‘जो आज्ञा’ कहकर मकान वाले से शिकायत करने चल देते। पर्वत चाहे बूंदों का आघात कितना ही सहें, लक्ष्मण बर्दाश्त नहीं करते। वे बाण मारकर बादलों को भगा देते या मकान-मालिक का ही शिरच्छेद कर देते।’ (3/16) 1
इसमें राम को उनकी मिथकीय दुनियां से निकालकर टपकने वाली छत के नीचे रहने वाले निम्नमध्यवर्गीय किराएदार के साथ कर दिया गया है। पुराण-गाथा या रोमांचक साहित्य हमें अपनी स्थिति से ऊपर उड़ा ले जाता है। यहाँ निम्नमध्यवर्गीय व्यक्ति की स्थिति पुराण, गाथा, मिथक को अपनी तरह बना लेती है। अपनी स्थिति का अविस्मरणीय आग्रह परसाई के व्यंग्य निबंधों की विशेषता है, वे मिथकों का उपयोग मिथक-भंजन के लिए करते हैं। इससे वर्तमान या वस्तुस्थिति उजागर होती है।
हम जानते हैं कि पौराणिक नायकों को वर्तमान में पहले भी लाया गया है, अब भी लाया जाता हैः ‘मानुस हौं तो बही कवि चोंच बसौं नित टेम्स नदी के किनारे/ ’जो पशु हौं तो बनौं बुलडाग चलौं नितकार में पूँछ निकारे/’ आदि में भी यही किया गया है। पौराणिक पात्रों को आधुनिक स्थितियों में डालकर, नए फैशन की हँसी उड़ाना हिंदी व्यंग्य में बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। लेकिन ऐसे लोग वर्तमानता को परसाई की तरह नहीं देखते। परसाई की दृष्टि द्वंद्वात्मक है। उनके यहाँ वर्तमानता एक ऐतिहासिक अवधारणा और मूल्य है। वे पौराणिक पात्रों की टक्कर प्रायः निम्नमध्यवर्गीय, अभावग्रस्त या शोभित पात्रों से कराते हैं। उनके यहाँ ये पौराणिक पात्र वर्तमान युग की जटिल विषमता में उलझकर अपनी पौराणिक गरिमा झाड़ देते हैं। अभावग्रस्त शोभित जन के प्रति बेहद करुणा ही परसाई को कबीर और गा़लिब से जोड़ती है। यह करुणा व्यंग्य में छिपी रहती है। परसाई को कबीर और गालिब से जोड़ती है। यह करुणा व्यंग्य में छिपी रहती है।
परसाई को कबीर और ग़ालिब से यों ही नहीं जोड़ा
1. (3/16) परसाई रचनावली, खंड 3, पृष्ठ 16 का सूचक है। आगे भी यही क्रम है।
परसाई को कबीर और ग़ालिब से यों ही नहीं जोड़ा जा रहा है। इस पर यथावसर चर्चा की जाएगी।
परसाई के लेखन को समग्रता में देखा जाए तो वर्तमान भारत के द्वंद्व का चित्र उभरेगा। इस चित्र में एक कसमसाता, छटपटाता हुआ भारत है जिसे एक और छद्म भारत ने दबोच रखा है। दबोचने वाला और दमित दोनों भारत सक्रिय हैं। दोनों के बीच निरंतर दाव-पेंच चल रहे हैं। शोषक-शोषित उनकी समस्याएँ, सांस्कृतिक, आर्थिक आचरण सब परम्पर संबद्ध हैं। इस सघन परम्परा-संबंधता को ही वर्तमानता की अखंडता समझिए। इससे उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग सब की आशाएँ, आकांक्षाएँ हैं। सबके अपने-अपने दुःख हैं। दुख और सुख विविध हैं, भिन्न हैं, परस्पर विरोधी हैं, छद्म हैं, सच्चे हैं।
‘मेरा दुख यह है कि मुझे बिजली का 40 रू. का बिल जमा करना है और मेरे पास इतने रुपए नहीं है।
तभी एक बंधु अपना दुख बताने लगता है। उसने 8 कमरों का मकान बनाने की योजना बनाई थी।6 कमरे बन चुके हैं। 2 के लिए पैसे की तंगी आ गयी है।
एक बंधु की रोटरी मशीन आ गयी है। अब मोनो मशीन आने में कठिनाई आ गई है। वे दुखी हैं।
एक जीवित रहने का संघर्ष है और एक संपन्नता का संघर्ष।’ (3/ 45-46)
सतर्क वैज्ञानिक-बोध परसाई की रचना का प्रधान साधक है। वे इस बोध से संस्थानों, रूढ़ियों, आचरण आदि के टुकड़े कर देते हैं और उनका व्यंग्य वास्तविकता प्रकट कर देता है। चूँकि अमानवीय है अतएव इसकी अनुभूति करुणा जगाती है।
स्वातंत्र्योत्तर भारत स्वाधीनता आंदोलन के सिद्धांत गायब नहीं हो गए हैं। उनका इस्तेमाल किया जाता है मुखौटों के रूप में। कथनी और करनी में भिन्नता नहीं, विपरीतता है। फलतः देश में मानवीय विरासत को मुखौटै के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह हमारे देश में ज्यादा आसान है क्योंकि हमारे देश की जनता का अधिकांश रूढ़िग्रस्त है। जो शिक्षित हैं उनकी आँखों पर भी रूढ़ि और अंधविश्वास का आवरण पड़ा है। जनता का शोषण करने वाली शक्तियाँ एक हो जाती हैं। सांप्रदायिकता, बहुराष्ट्रीय पूँजी, फासिज्म, धर्म, वर्ग-विभाजन को बरकरार रखने वाली राजनीतिक शक्तियाँ सब इस नाटकीय षड्यंत्र में शामिल होकर एक जुट हो जाती हैं।
राजनीतिज्ञ स्वाधीनता आंदोलन के नारों-सत्य, अहिंसा, सेवा को, धर्माधिकारी अतीत को, फासिज्म संस्कृति को मुखौटा बनाते हैं तो देशी पूँजीवाद और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ सब कुछ इस्तेमाल विज्ञापन के रूप में करती हैं। विज्ञापन हमारे युग का सबसे बड़ा और घातक मुख़ौटा है। वह आर्थिक शोषण के लिए राजनैतिक, चरित्र, संस्कृति, मानसिकता को विकृत करता है। नारी को शारीरिकता में सीमित करता है। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि पूँजीवाद सामंती दृष्टि का ही विकास है। इसके लिए क्षणवाद एवं व्यक्तिवादी अनुभववाद सहायक होते हैं।
परसाई यह सारा छद्म देख लेते हैं तो इसका श्रेय उस वैज्ञानिक दृष्टि को भी है जो पूँजीवादी के विरोध में समाजवादी विकास का विकल्प प्रस्तुत करती है। साम्राज्यवाद से समर्पित, कभी-कभी उससे अपने स्वार्थ के लिए टकराता हुआ भी, देशी पूँजीवीद और अनेकता के साथ एकता में विश्वास करने वाला समाजवाद-इन दोनों का परस्पर विरोध हमारे युग की वर्तमानता का अंतर्विरोधी है। इसे हमारे देश का प्रत्येक जन झेल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति इस संघर्ष-गाथा का पात्र है। हम जब आँकड़ों का सिद्धांतों की भाषा में बहस करते हैं, तब इस संघर्ष गाथा की अनुभव धार बहुत कुछ अरूप होकर ओझल हो जाती है। देश के एक-एक जन का दुःख अनुभव अपने आप में अखंड है। इन सबके अनुभवों को एक साथ देखने का प्रयास करने वाला रचनाकार अपने युग का महाकाव्य लिखता है। इस व्याप्ति में प्रत्येक का संघर्ष ओझल नहीं होता। यही वर्तमानता है। मुक्तिबोध पीड़ा में जो व्याप्ति है, वह दृष्टव्य हैः
मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में
चमकता हीरा है,
हर एक छाती में आत्मा अधीरा है
प्रत्येक सुस्मित में विमल सदानीरा है
मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में
महाकाव्य पीड़ा है
दुःख की कथाएँ, तरह-तरह की शिकायतें,
अहंकार विश्लेषण, चारित्रिक आख्यान,
जमाने के जानदार सूरें व आयतें
सुनने को मिलती हैं।
चमकता हीरा है,
हर एक छाती में आत्मा अधीरा है
प्रत्येक सुस्मित में विमल सदानीरा है
मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में
महाकाव्य पीड़ा है
दुःख की कथाएँ, तरह-तरह की शिकायतें,
अहंकार विश्लेषण, चारित्रिक आख्यान,
जमाने के जानदार सूरें व आयतें
सुनने को मिलती हैं।
यही महाकाव्य-पीड़ा परसाई की रचना में हैं उसका रूप है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में कथनी-करनी की विपरीतता और नाटकीयता उत्पन्न की है, वह उनके व्यंग्य-निबंधों में है। लेकिन इस विपरीतता और नाटकीयता में सफल शोषकों का स्वांग और अभावग्रस्त जन की पीड़ा है। इस पीड़ा का विभावन है।
यह पीड़ा-बोध परसाई के सौंदर्य-बोध का अंग है। वे व्यंग्य के पैने हथियार से हमारी अमानवीयता और कमजोरियों को छील-छीलकर नैतिक दृष्टि से अधिक विकसित मनुष्य को गढ़ते हैं। उनका सतर्क बोध उनके व्यंग्य को वैज्ञानिक नैतिकता और सौंदर्य-बोध से जोड़ता है। यह बोध वर्तमानता की पर्तों और नाटकीयता है। वह विभिन्न मनोविकारों को संबद्ध करके करुणा की भूमि का विस्तार करता है। इन सबसे परसाई का व्यंग्य अधिक जटिल बनता है। वह पहले की अपेक्षा अधिक मनोविकारों और जीवन स्थितियों से संपृक्त है। उनका व्यंग्य अधिक अर्थ-भूमि पर स्थिति है, वह अधिक भाव-भूमि घेरता है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में कहें तो परसाई के व्यंग्य से मनोविकारों का ‘व्यायाम’ होता है।
व्यंग्य विषमता पर आधारित होता है, वह चोट भी विषमता पर करता है। विषमता का विलोम सुषमा है-सुषमा सौंदर्य उत्पन्न करती है। सुषमा को औचित्य भी कह सकते हैं, जो जहाँ जितना होना चाहिए वह वहाँ उतना है तो उससे सौंदर्य उत्पन्न होगा। नहीं है-अनौचित्य है तो विषमता होगी-यही कुरुपता है। इससे हास्य उपन्न होता है। ‘व्यंग्य’ शब्द में विकलांगता का भाव है। जिस प्रकार स्थूल और शारीरिक विषमता होती है उसी प्रकार सामाजिक और आचरणगत भी। घटिया लोग लंबी नाक, मोटी तोंद, हकलाहट, विकलांगता की हँसी उड़ाकर अपने को रचनाकार समझते हैं। ऐसा व्यंग्य (?) हिंदी की रंग-बिरंगी पत्रिकाओं में खपा रहता है। यह उसी प्रकार का छिछोरापन है जैसा कि चटक-मटक, बाँकी अदा, पतली कमर पर फिदा हो जाना। ऐसी हँसी मानवीयता नहीं पशुता की पहचान है। यह बात पशुओं में नहीं मानव-पशुओं में पाई जाती है। वे लँगड़े आदमी की विकंलागता पर हँसते हैं, उनकी हँसी से आदमी को कितनी तकलीफ हो रही है, इस पर ध्यान नहीं देते। इतिहास में अमानवीय हँसी के दारुण उदाहरण हैं। कहते हैं कि रोमन लोग एकत्र होकर युद्ध बंदियों के सामने भूखे शेरों को छोड़ देते थे। यह उनका मनोरंजन था। नीरो रोम को आग की लपटों में देख रहा था और वायलिन बजा रहा था। वह अपनी जातीय परम्परा का ही निर्वाह कर रहा था। दुःखी आदमी पर हँसना, उस पर ईंट-पत्थर चलाने जैसा है। पीड़ा-व्यथा पर खल हँसना ही जानते हैं। मीरा ने लिखा-
यह पीड़ा-बोध परसाई के सौंदर्य-बोध का अंग है। वे व्यंग्य के पैने हथियार से हमारी अमानवीयता और कमजोरियों को छील-छीलकर नैतिक दृष्टि से अधिक विकसित मनुष्य को गढ़ते हैं। उनका सतर्क बोध उनके व्यंग्य को वैज्ञानिक नैतिकता और सौंदर्य-बोध से जोड़ता है। यह बोध वर्तमानता की पर्तों और नाटकीयता है। वह विभिन्न मनोविकारों को संबद्ध करके करुणा की भूमि का विस्तार करता है। इन सबसे परसाई का व्यंग्य अधिक जटिल बनता है। वह पहले की अपेक्षा अधिक मनोविकारों और जीवन स्थितियों से संपृक्त है। उनका व्यंग्य अधिक अर्थ-भूमि पर स्थिति है, वह अधिक भाव-भूमि घेरता है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में कहें तो परसाई के व्यंग्य से मनोविकारों का ‘व्यायाम’ होता है।
व्यंग्य विषमता पर आधारित होता है, वह चोट भी विषमता पर करता है। विषमता का विलोम सुषमा है-सुषमा सौंदर्य उत्पन्न करती है। सुषमा को औचित्य भी कह सकते हैं, जो जहाँ जितना होना चाहिए वह वहाँ उतना है तो उससे सौंदर्य उत्पन्न होगा। नहीं है-अनौचित्य है तो विषमता होगी-यही कुरुपता है। इससे हास्य उपन्न होता है। ‘व्यंग्य’ शब्द में विकलांगता का भाव है। जिस प्रकार स्थूल और शारीरिक विषमता होती है उसी प्रकार सामाजिक और आचरणगत भी। घटिया लोग लंबी नाक, मोटी तोंद, हकलाहट, विकलांगता की हँसी उड़ाकर अपने को रचनाकार समझते हैं। ऐसा व्यंग्य (?) हिंदी की रंग-बिरंगी पत्रिकाओं में खपा रहता है। यह उसी प्रकार का छिछोरापन है जैसा कि चटक-मटक, बाँकी अदा, पतली कमर पर फिदा हो जाना। ऐसी हँसी मानवीयता नहीं पशुता की पहचान है। यह बात पशुओं में नहीं मानव-पशुओं में पाई जाती है। वे लँगड़े आदमी की विकंलागता पर हँसते हैं, उनकी हँसी से आदमी को कितनी तकलीफ हो रही है, इस पर ध्यान नहीं देते। इतिहास में अमानवीय हँसी के दारुण उदाहरण हैं। कहते हैं कि रोमन लोग एकत्र होकर युद्ध बंदियों के सामने भूखे शेरों को छोड़ देते थे। यह उनका मनोरंजन था। नीरो रोम को आग की लपटों में देख रहा था और वायलिन बजा रहा था। वह अपनी जातीय परम्परा का ही निर्वाह कर रहा था। दुःखी आदमी पर हँसना, उस पर ईंट-पत्थर चलाने जैसा है। पीड़ा-व्यथा पर खल हँसना ही जानते हैं। मीरा ने लिखा-
मेरो मरण औ जग केरी हाँसी।
यह हँसी दुख को और तीव्र कर देती है, यानी उसे और असहनीय बना देती है। संवेदनशील प्राणी के लिए यह हँसी कैसी होती है, इसकी व्यंजना निराला कि इन पंक्तियों में हैः
‘दूबर होत नहीं कबहूँ पकवान के विप्र मसान के कूकुर’ की सार्थकता मैंने मित्रों में देखी, जिनकी निगाह दूसरों की दुनिया की लाश पर थी। वे पहले फटीचर थे, पर अब अमीर बन गये हैं, दोमंज़िला मकान खड़ा कर लिया है, मोटर पर सैर करते है, मुझे देखते हैं जैसे मेरा-उनका नौकर-मालिक का रिश्ता हो। नक्की स्वरों में कहते हैं-हाँ, अच्छा है; ज़रा सनकी है। फिर बड़े गहरे पैठकर मित्र के साथ हँसते हैं।’ (देवी)
हँसी खलों को ही नहीं आती। कबीर को भी आती थी। कबीरदास को हँसी भी आती है और रोना भी आता है। लोग झूठी सफलता पर इतराते हैं, मूर्ख और ज्ञानियों की मुद्रा अपनाते हैं, जानते कुछ नहीं और बखानते ज्यादा हैं तो कबीरदास को हँसी आती है। अज्ञानता के कारण लोग भटकते हैं, परेशान होते हैं तो कबीरदास उदास होते हैं, कभी-कभी रो भी देते हैं। कबीरदास की हँसी उनके रोने से जुड़ी है। जो सांसारिक दृष्टि से सफल हैं, झूठे सुख को सुख समझकर पुलकित हैं उन पर कबीरदास हँसते हैं, सामान्य लोगों के भ्रम पर वे उदास होते हैं या रोते हैं। हास्य और करुणा का यह मेल कबीर की मानवीयता के कारण है।
हँसता वह है जो अपने आप को उचित या सुरक्षित समझता है। वह दूसरों की हँसी उड़ाता है। मायाग्रस्त लोग अज्ञानी हैं। वे असुरक्षित हैं, तब भी हँसते हैं। हास्यास्पद दूसरों की हँसी उड़ाए तो उसकी हास्यास्पदता बहुत बढ़ जाती है। कबीरदास ऐसे लोगों से कहते हैं- बहुत जमा कर लिया है, समझते हो सब कुछ ‘मेरा है।’ यमराज का डंडा मूँड़ पर लगते ही फैसला हो जाएगा कि तुम्हारा क्या हैः
‘दूबर होत नहीं कबहूँ पकवान के विप्र मसान के कूकुर’ की सार्थकता मैंने मित्रों में देखी, जिनकी निगाह दूसरों की दुनिया की लाश पर थी। वे पहले फटीचर थे, पर अब अमीर बन गये हैं, दोमंज़िला मकान खड़ा कर लिया है, मोटर पर सैर करते है, मुझे देखते हैं जैसे मेरा-उनका नौकर-मालिक का रिश्ता हो। नक्की स्वरों में कहते हैं-हाँ, अच्छा है; ज़रा सनकी है। फिर बड़े गहरे पैठकर मित्र के साथ हँसते हैं।’ (देवी)
हँसी खलों को ही नहीं आती। कबीर को भी आती थी। कबीरदास को हँसी भी आती है और रोना भी आता है। लोग झूठी सफलता पर इतराते हैं, मूर्ख और ज्ञानियों की मुद्रा अपनाते हैं, जानते कुछ नहीं और बखानते ज्यादा हैं तो कबीरदास को हँसी आती है। अज्ञानता के कारण लोग भटकते हैं, परेशान होते हैं तो कबीरदास उदास होते हैं, कभी-कभी रो भी देते हैं। कबीरदास की हँसी उनके रोने से जुड़ी है। जो सांसारिक दृष्टि से सफल हैं, झूठे सुख को सुख समझकर पुलकित हैं उन पर कबीरदास हँसते हैं, सामान्य लोगों के भ्रम पर वे उदास होते हैं या रोते हैं। हास्य और करुणा का यह मेल कबीर की मानवीयता के कारण है।
हँसता वह है जो अपने आप को उचित या सुरक्षित समझता है। वह दूसरों की हँसी उड़ाता है। मायाग्रस्त लोग अज्ञानी हैं। वे असुरक्षित हैं, तब भी हँसते हैं। हास्यास्पद दूसरों की हँसी उड़ाए तो उसकी हास्यास्पदता बहुत बढ़ जाती है। कबीरदास ऐसे लोगों से कहते हैं- बहुत जमा कर लिया है, समझते हो सब कुछ ‘मेरा है।’ यमराज का डंडा मूँड़ पर लगते ही फैसला हो जाएगा कि तुम्हारा क्या हैः
जम का डंड मूँड़ महि लागै पल मा होई निबेरा।
कबीरदास राम के भरोसे अपने को सुरक्षित और सांसारिक दृष्टि से सफल किंतु राम-विमुख लोगों की मूर्खता पर हँसते थे। इस व्यंग्य का तर्क और बोध था। वह जाग्रत व्यक्ति का व्यंग्य था उनका व्यंग्य करुणा से स्पंदित था। वह लोकोन्मुख भी था।, पक्षधर था–भक्तों और पीड़ित प्राणियों के पक्ष में कबीर जागते हैं, दुखी हैं और रोते हैं:
सुखिया सब संसार है खावै औ सोवै।
दुखिया दास कबीर है जागै औ रोवै।।
दुखिया दास कबीर है जागै औ रोवै।।
जागना बोध है, रोना करुणावान् होना है, दुखी होना संवेदनशील होना है। जिस तरह व्यंग्य का तर्क और बोध है उसी प्रकार दुखी होने और रोने का भी। यह वही कबीर दास हैं जो बेहद्दी मैदान में सोते हैं, जो काम ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं कर पाए यानी अपनी चादर को निर्मल न रख सके, उसे ‘जस का तस’ धर देने वाले हैं। यह अखंड विश्वास, हास्य-व्यंग्य करुणा- सब उनके मानसिक ढाँचे के विविध किंतु अंतस्संबंधित पहलू हैं। मानसिक ढाँचे की इस समग्रता को ही उनकी भक्ति कहनी चाहिए। हरिशंकर परसाई के व्यंग्य का आधार इतिहास बोध है। यह इतिहास बोध उनकी समस्त रचनात्मकता में सक्रिय है। यही उन्हें वह औचित्य और सुरक्षा प्रदान करता है जिसके भरोसे वे व्यंग्य कर सकते हैं और समाज-विरोधियों पर हँस सकते हैं। कबीर परमसत्ता की साधना करते थे, वे काल को चीरकर कालातीत स्थिति में पहुँचने का रास्ता खोजत थे। फिर भी ‘मूरों’ (गुलामों को बेचनेवाले सौदागरों) के लिए नहीं, ‘बंदियों’ (जिन्हें गुलाम के रूप में बेचा जाता था) के लिए रोने की बात करते थे-
मूरों को का रोइए जे़ अपने घर जाहिं।
रोइए बंदी जनन को जे हाटहिं-हाट बिकाहिं।।
रोइए बंदी जनन को जे हाटहिं-हाट बिकाहिं।।
परसाई समाजवाद में विश्वास करते हैं। वे वर्ग-विभक्त समाज में दूसरों का हक छीनकर सांसारिक सफलता प्राप्त करने की अमानवीयता एवं टुच्चेपन को समझते हैं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book