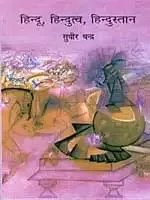|
लेख-निबंध >> हिन्दू हिन्दुत्व हिन्दुस्तान हिन्दू हिन्दुत्व हिन्दुस्तानसुधीर चन्द्र
|
429 पाठक हैं |
||||||
सारे बौद्धिक प्रयत्न के बावजूद, ‘हिन्दू अवचेतन’ अपने को ही भारतीय मानता है।
Hindu Hindutva Hindustan-
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
सारे बौद्धिक प्रयत्न के बावजूद, ‘हिन्दू अवचेतन’ अपने को ही भारतीय मानता है। भारत जैसे बहुधर्मी और सांस्कृतिक वैविध्य से भरपूर देश के लिए ऐसी मान्यता अनिवार्यतः अनिष्टकारी है। पिछले कुछ समय से यह मान्यता अवचेतन से निकलकर उत्तरोत्तर आक्रामक होती जा रही है। बौद्धिक प्रयत्न के बावजूद नहीं, बल्कि खुलकर एक विचारधारा के रूप में यह हिन्दू को ही राष्ट्र मान बैठी है।
खतरा यदि प्रधानतः विचारधारा और उससे जुड़ी किसी राजनीतिक पार्टी का होता तो उससे जूझना मुश्किल न होता। पर आज परेशानी यह है कि ‘हिन्दू अवेचतन’ कहीं न कहीं उन बातों को अपनी अँधेरी गहराइयों में मानता है जिनको चेतना के स्तर पर वह राष्ट्र के लिए घातक और नैतिक रूप से अवांछनीय समझता है। जरूरी है कि उसका सामना इस दुनिया से कराया जाए।
बगैर इस आत्म-साक्षात्कार के वह उन प्रवंचनों से मुक्त नहीं हो सकेगा जो उसको यह नहीं समझने देतीं कि ‘वन्दे मातरम्’ एक स्तर पर बन्दनीय होते हुए भी एक दूसरे स्तर पर एक ऐसी राजनीति का अस्त्र मात्र है जहाँ सत्ता ही परम ध्येय है, जन कल्याण का माध्यम नहीं।
खतरा यदि प्रधानतः विचारधारा और उससे जुड़ी किसी राजनीतिक पार्टी का होता तो उससे जूझना मुश्किल न होता। पर आज परेशानी यह है कि ‘हिन्दू अवेचतन’ कहीं न कहीं उन बातों को अपनी अँधेरी गहराइयों में मानता है जिनको चेतना के स्तर पर वह राष्ट्र के लिए घातक और नैतिक रूप से अवांछनीय समझता है। जरूरी है कि उसका सामना इस दुनिया से कराया जाए।
बगैर इस आत्म-साक्षात्कार के वह उन प्रवंचनों से मुक्त नहीं हो सकेगा जो उसको यह नहीं समझने देतीं कि ‘वन्दे मातरम्’ एक स्तर पर बन्दनीय होते हुए भी एक दूसरे स्तर पर एक ऐसी राजनीति का अस्त्र मात्र है जहाँ सत्ता ही परम ध्येय है, जन कल्याण का माध्यम नहीं।
उपक्रम
हिन्दुत्व के दौर में हिन्दू, और भारतीय, होने के दायित्व से जूझते हैं ये लेख। इनके लेखक का इस विषय से पुराना संबंध है। मुख्तसर कुछ ऐसा :
एक वक्त था- देश के कुछ हिस्सों में आज भी है- जब किसी भी अजनबी से शुरूआती बातचीत नाम और गाँव के बाद सहज ही जाती थी जाति पर, ‘कौन बाम्हन हैं आप ?’ आश्चर्य नहीं बचपन में बड़ा अभिमान था अपनी जातीयता का। घुट्टी में ही मिल गया था विश्वास- जो, आश्चर्य है, शीशे से भी डिगा- कि सुन्दर सुडौल होते हैं हम सजातीय, और साथ ही तीक्ष्ण बुद्धि, हास्यप्रिय, रसिक, इत्यादि, इत्यादि।
गाढ़े संबंध रहे अन्य जाति और धर्मवालों से भी। बाबा गांधीवादी थे। सो जातीय एवं धार्मिक संकीर्णता से बच गया। छुआछूत से भी। मुसलमानों से खसूसन अच्छे रिश्ते बने। मुहर्रम में ताज़िये रुकते थे हमारे मुहल्ले के कोने पर, और बाबा की अगुआई में आगे बढ़ते थे। दोनों भाई बड़े हुए, माँ को अम्मी कहते। आस-पड़ोस में भी माँ इसी संबोधन से जानी जानें लगीं। आज भी वैसे ही जानी जाती हैं। सगी मौसियों से कम नहीं थीं सुगरा मौसी, बनारस के बड़े हकीम साहब की बेगम। पिता का तबादला एक बार कॉलिज खुलने के बाद हुआ, और बरेली कॉलिज के इकलौते छात्रावास में कोई कमरा खाली था नहीं, तो महमूदुल हसन चाचाजी ने बेटे की तरह अपने साथ रखा।
फिर शिक्षा ने रंग दिखाया। परेशानी-सी होने लगी अपनी ब्राह्मण-हिन्दू पहचान से। हाईस्कूल का फॉर्म भरते समय अपना जाति-सूचक नाम हटा दिया गया। बाद में खासा उग्र रूप ले गई यह परेशानी और बन गई सुसंगत विचारधारा। काफी लम्बा चला जाति व धर्म के सैद्धान्तिक विरोध का दौर।
काफी बाद में, धीरे-धीरे आनी शुरू हुई समझ की तमाम पहचानों का पेचीदा और नित बदलता चक्रव्यूह होता है हमारा व्यक्तित्व। यह भी कि स्वस्थ सामाजिक-नागरिक जीवन की निर्मिति इसमें से कुछ पहचानों के नकार से नहीं, उनकी सम्यक् स्थिति से होती है। होनी चाहिए।
यही समझ एक नैतिक दायित्व-सी उबरने लगी 1984 से जब सिखों के विरुद्ध पलक झपकते उमड़ उठी हिंसा को देखा देश की राजधानी में। और गहराई आडवाणी की रथयात्रा के साथ हुए उग्र राजनैतिक हिन्दुत्व का उद्घोष के फलस्वरूप।
अन्दर का हिन्दू फिर जागा। हिन्दू और भारतीय, मैं हूँ, और मेरे जैसे अनगिनत लोग, न कि आडवाणी अथवा उनके अनुगामी।
फिर भी, आक्रामक हिन्दुत्व की सारी भयावहता के बावजूद, गुजरात 2002 अल्पकालीन ही था। कहाँ ले जा रही है यह डरावनी इक्कीसवीं सदी ?
1984 से 2002 के बीच लिखे गए इन लेखों में कोशिश है संशय और हस्तक्षेप के बीच तनी रस्सी पर चलने की। संशय यह है कि अन्दर और बाहर का घमासान पकड़ में नहीं आता। किन्तु उस कारण निष्क्रिय तो नहीं बैठ सकते हम। क्योंकर तब ही चीज़ों को इच्छित दिशा में बदलने का उपक्रम ? क्या हो सकता है उस हस्तक्षेप का औचित्य एवं आधार ?
संशय और हस्तक्षेप दोनों की ही अनिवार्यता से उपजे द्वन्द्व की तात्विक चर्चा नहीं करते ये लेख। गांधी के ‘हर कोई अपने को देखे’ की याद करते, ये कभी अपने अन्दर की और बाहर की तारीकियों से जूझते हैं, और महसूस करते हैं कि अन्दर और बाहर अलग नहीं है, एक दूसरे में बिंधे हैं, ऐसे कि अलग न हो सकें।
एक अनुपस्थिति है इन लेखों में। उसकी पड़ताल मैं खुद ढंग से नहीं कर पाया हूँ। पर उसका जिक्र न करने से अपने को परखते हुए बाहर देखने की भावना दूषित होगी। कश्मीरी पंडित अनुपस्थित हैं यहाँ। एक प्रतीक के रूप में ‘सोमनाथ’ से जुड़ी मानसिकता को समझ सका मैं, 1984 और अयोध्या के झकझोरा, गोधरा कांड से उद्वेलित हुआ और उसके बाद की नृशंसता ने तो हिला ही डाला। कशमीरी पंडितों की व्यथा से कैसे अछूता रह गया मैं ?
इस सवाल का अवश्य ही राजनैतिक, सामरिक महत्त्व है। उतना ही होता तो मुश्किल नहीं था कशमीरी पंडितों पर दो आँसू बहा देना। उससे कहीं गहरा, सवाल मानवीयता का है। कैसे होता है कि एक समुदाय का दर्द ही नहीं दिखता हमें ? धर्मनिरपेक्षता भी तो, मानवीय होने के नाते, स्खलित होती है उस दर्द के प्रति उदासीनता से।
हिन्दी में यह मेरी पहली पुस्तक है। तहेदिल से आभार जताना चाहता हूँ सर्वश्री अशोक वाजपेयी, नामवर सिंह, राजकिशोर, ओम थानवी, मंगलेश डबराल, परमानन्द श्रीवास्तव, पियूष दइया तथा अशोक महेश्वरी के प्रति जिन्होंने मातृभाषा की ओर मोड़ा मुझे।
आभार गुलाम मोहम्मद शेख़ का भी जिन्होंने बड़े स्नेह से अपनी ऐसे सशक्त रचना कवर के लिए उपलब्ध कराई।
अन्त में, जानता हूँ कि जिन्दगी भर के हमारे प्रेम को इसकी दरकार नहीं, पर विनोद भैया और भाभी को यह पुस्तक समर्पित करते हुए बड़ा सुख हो रहा है।
एक वक्त था- देश के कुछ हिस्सों में आज भी है- जब किसी भी अजनबी से शुरूआती बातचीत नाम और गाँव के बाद सहज ही जाती थी जाति पर, ‘कौन बाम्हन हैं आप ?’ आश्चर्य नहीं बचपन में बड़ा अभिमान था अपनी जातीयता का। घुट्टी में ही मिल गया था विश्वास- जो, आश्चर्य है, शीशे से भी डिगा- कि सुन्दर सुडौल होते हैं हम सजातीय, और साथ ही तीक्ष्ण बुद्धि, हास्यप्रिय, रसिक, इत्यादि, इत्यादि।
गाढ़े संबंध रहे अन्य जाति और धर्मवालों से भी। बाबा गांधीवादी थे। सो जातीय एवं धार्मिक संकीर्णता से बच गया। छुआछूत से भी। मुसलमानों से खसूसन अच्छे रिश्ते बने। मुहर्रम में ताज़िये रुकते थे हमारे मुहल्ले के कोने पर, और बाबा की अगुआई में आगे बढ़ते थे। दोनों भाई बड़े हुए, माँ को अम्मी कहते। आस-पड़ोस में भी माँ इसी संबोधन से जानी जानें लगीं। आज भी वैसे ही जानी जाती हैं। सगी मौसियों से कम नहीं थीं सुगरा मौसी, बनारस के बड़े हकीम साहब की बेगम। पिता का तबादला एक बार कॉलिज खुलने के बाद हुआ, और बरेली कॉलिज के इकलौते छात्रावास में कोई कमरा खाली था नहीं, तो महमूदुल हसन चाचाजी ने बेटे की तरह अपने साथ रखा।
फिर शिक्षा ने रंग दिखाया। परेशानी-सी होने लगी अपनी ब्राह्मण-हिन्दू पहचान से। हाईस्कूल का फॉर्म भरते समय अपना जाति-सूचक नाम हटा दिया गया। बाद में खासा उग्र रूप ले गई यह परेशानी और बन गई सुसंगत विचारधारा। काफी लम्बा चला जाति व धर्म के सैद्धान्तिक विरोध का दौर।
काफी बाद में, धीरे-धीरे आनी शुरू हुई समझ की तमाम पहचानों का पेचीदा और नित बदलता चक्रव्यूह होता है हमारा व्यक्तित्व। यह भी कि स्वस्थ सामाजिक-नागरिक जीवन की निर्मिति इसमें से कुछ पहचानों के नकार से नहीं, उनकी सम्यक् स्थिति से होती है। होनी चाहिए।
यही समझ एक नैतिक दायित्व-सी उबरने लगी 1984 से जब सिखों के विरुद्ध पलक झपकते उमड़ उठी हिंसा को देखा देश की राजधानी में। और गहराई आडवाणी की रथयात्रा के साथ हुए उग्र राजनैतिक हिन्दुत्व का उद्घोष के फलस्वरूप।
अन्दर का हिन्दू फिर जागा। हिन्दू और भारतीय, मैं हूँ, और मेरे जैसे अनगिनत लोग, न कि आडवाणी अथवा उनके अनुगामी।
फिर भी, आक्रामक हिन्दुत्व की सारी भयावहता के बावजूद, गुजरात 2002 अल्पकालीन ही था। कहाँ ले जा रही है यह डरावनी इक्कीसवीं सदी ?
1984 से 2002 के बीच लिखे गए इन लेखों में कोशिश है संशय और हस्तक्षेप के बीच तनी रस्सी पर चलने की। संशय यह है कि अन्दर और बाहर का घमासान पकड़ में नहीं आता। किन्तु उस कारण निष्क्रिय तो नहीं बैठ सकते हम। क्योंकर तब ही चीज़ों को इच्छित दिशा में बदलने का उपक्रम ? क्या हो सकता है उस हस्तक्षेप का औचित्य एवं आधार ?
संशय और हस्तक्षेप दोनों की ही अनिवार्यता से उपजे द्वन्द्व की तात्विक चर्चा नहीं करते ये लेख। गांधी के ‘हर कोई अपने को देखे’ की याद करते, ये कभी अपने अन्दर की और बाहर की तारीकियों से जूझते हैं, और महसूस करते हैं कि अन्दर और बाहर अलग नहीं है, एक दूसरे में बिंधे हैं, ऐसे कि अलग न हो सकें।
एक अनुपस्थिति है इन लेखों में। उसकी पड़ताल मैं खुद ढंग से नहीं कर पाया हूँ। पर उसका जिक्र न करने से अपने को परखते हुए बाहर देखने की भावना दूषित होगी। कश्मीरी पंडित अनुपस्थित हैं यहाँ। एक प्रतीक के रूप में ‘सोमनाथ’ से जुड़ी मानसिकता को समझ सका मैं, 1984 और अयोध्या के झकझोरा, गोधरा कांड से उद्वेलित हुआ और उसके बाद की नृशंसता ने तो हिला ही डाला। कशमीरी पंडितों की व्यथा से कैसे अछूता रह गया मैं ?
इस सवाल का अवश्य ही राजनैतिक, सामरिक महत्त्व है। उतना ही होता तो मुश्किल नहीं था कशमीरी पंडितों पर दो आँसू बहा देना। उससे कहीं गहरा, सवाल मानवीयता का है। कैसे होता है कि एक समुदाय का दर्द ही नहीं दिखता हमें ? धर्मनिरपेक्षता भी तो, मानवीय होने के नाते, स्खलित होती है उस दर्द के प्रति उदासीनता से।
हिन्दी में यह मेरी पहली पुस्तक है। तहेदिल से आभार जताना चाहता हूँ सर्वश्री अशोक वाजपेयी, नामवर सिंह, राजकिशोर, ओम थानवी, मंगलेश डबराल, परमानन्द श्रीवास्तव, पियूष दइया तथा अशोक महेश्वरी के प्रति जिन्होंने मातृभाषा की ओर मोड़ा मुझे।
आभार गुलाम मोहम्मद शेख़ का भी जिन्होंने बड़े स्नेह से अपनी ऐसे सशक्त रचना कवर के लिए उपलब्ध कराई।
अन्त में, जानता हूँ कि जिन्दगी भर के हमारे प्रेम को इसकी दरकार नहीं, पर विनोद भैया और भाभी को यह पुस्तक समर्पित करते हुए बड़ा सुख हो रहा है।
15 अप्रैल, 2003
-सुधीर चन्द्र
दायित्व संशय और हस्तक्षेप का
जानने, खासतौर से अपने समय को जानने, की कठिनाई को हम सब जानते हैं। जानने और न जानने की अनिश्चितता में जीवन बीत जाता है। इसी अनिश्चितता में होते हैं हमारे सारे निश्चय, निर्णय और संकल्प। तथा पनपते हैं हमारे सारे मूल्य, सारे विचार, सारी आस्थाएँ, सारे विश्वास, सारे पूर्वग्रह। सब परिवर्तनशील। पर हम भूले रहते हैं अपनी निर्मिति की निरंतरता को, और अपने अन्दर आए दिन बनते-बिगड़ते पृथक, परस्पर विरोधी तत्वों के तालमेल को। प्राय: बने रहते हैं अपने तात्क्षणिक विश्वासों के प्रति आश्वस्त, अडिग। मानो अपनी वैचारिक शुद्घता की प्रतीति में ही निहित हो एहसास अपने होने का। जैसे उसके बिना हम अपने तईं साबुत ही न हों। न ही समाज के तईं।
ऐसे में अपने संशय से साक्षात्कार एक आवश्यक चुनौती बन जाता है। विरोधी विचारों व मान्यताओं के मध्य सम्वाद बनाए रखने की चुनौती। एक ऐसी चुनौती भी जो कहीं गहरे में हमारा सामना उस सम्वाद से कराती है जो हमारे अन्दर चलता रहता है और जिसके प्रति सचेत न रहना हमारी प्रवृत्ति-सा बन गया है। व्यक्ति और समष्टि दोनों के लिए आवश्यक प्रवृत्ति। ये तमाम सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं अन्य व्यवस्थित समूह, जिनके हम चाहे या अनचाहे सदस्य बनते हैं, कमोबेश, अपने-अपने निर्धारित सोच के ढाँचों में हमें बाँधते हैं। उदार, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था वाले समूह निस्बतन कम, अन्य कुछ ज्यादा। अवश्य ही, हमारे आन्तरिक व बाह्य जगत में संशय की ऐसी विराट उपस्थिति के बावजूद-या उसी के कारण-सच्चे-झूठे विश्वास का बने रहना व्यक्ति और समाज की कोई ज़बरदस्त ज़रूरत है।
इस अमूर्त, अपर्याप्त, संशय-प्रशस्ति के उपरान्त ‘अपने’ सन्देह का ज़िक्र। और उसकी शुरूआत विश्वास से। किंचित उससे भी अधिक, विश्वासजनित आक्रोश से। वैसे तो, कम-से-कम एक खास उम्र के लोगों के लिए, देश और दुनिया का कुछ समय से ऐसा ढर्रा रहा है कि उदासीनता या कभी-कभार क्षोभ से ज्यादा कोई प्रतिक्रिया हो नहीं पाती। ऐसे में आक्रोश अथवा क्रोध की अनुभूति बड़ी प्रीतिकर लगती है। अपने और समाज को लेकर आश्वासक।
हाल ही महसूस हुए इस आक्रोश का कारण था एक गर्
ऐसे में अपने संशय से साक्षात्कार एक आवश्यक चुनौती बन जाता है। विरोधी विचारों व मान्यताओं के मध्य सम्वाद बनाए रखने की चुनौती। एक ऐसी चुनौती भी जो कहीं गहरे में हमारा सामना उस सम्वाद से कराती है जो हमारे अन्दर चलता रहता है और जिसके प्रति सचेत न रहना हमारी प्रवृत्ति-सा बन गया है। व्यक्ति और समष्टि दोनों के लिए आवश्यक प्रवृत्ति। ये तमाम सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं अन्य व्यवस्थित समूह, जिनके हम चाहे या अनचाहे सदस्य बनते हैं, कमोबेश, अपने-अपने निर्धारित सोच के ढाँचों में हमें बाँधते हैं। उदार, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था वाले समूह निस्बतन कम, अन्य कुछ ज्यादा। अवश्य ही, हमारे आन्तरिक व बाह्य जगत में संशय की ऐसी विराट उपस्थिति के बावजूद-या उसी के कारण-सच्चे-झूठे विश्वास का बने रहना व्यक्ति और समाज की कोई ज़बरदस्त ज़रूरत है।
इस अमूर्त, अपर्याप्त, संशय-प्रशस्ति के उपरान्त ‘अपने’ सन्देह का ज़िक्र। और उसकी शुरूआत विश्वास से। किंचित उससे भी अधिक, विश्वासजनित आक्रोश से। वैसे तो, कम-से-कम एक खास उम्र के लोगों के लिए, देश और दुनिया का कुछ समय से ऐसा ढर्रा रहा है कि उदासीनता या कभी-कभार क्षोभ से ज्यादा कोई प्रतिक्रिया हो नहीं पाती। ऐसे में आक्रोश अथवा क्रोध की अनुभूति बड़ी प्रीतिकर लगती है। अपने और समाज को लेकर आश्वासक।
हाल ही महसूस हुए इस आक्रोश का कारण था एक गर्
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book