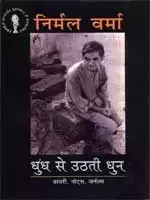|
यात्रा वृत्तांत >> धुंध से उठती धुन धुंध से उठती धुननिर्मल वर्मा
|
377 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है यात्रा-संस्मरण
Dhundh Se Uthati Dhun
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
हिन्दी कहानी और उपन्यास को नया मोड़ देने में निर्मल वर्मा को अपने जीवन-काल में ‘क्लासिक’ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। किन्तु अपनी सृजन यात्रा में एक सम्पूर्ण गद्यकार की हैसियत से उन्होंने गद्य की अन्य विद्याओं को ऐसी विचारात्मक गरिमा और ऊर्जा प्रदान की है, जिसमें आधुनिक हिन्दी का समूचा ‘गद्य-काल’ समृद्ध हुआ है। डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में, निर्मल वर्मा के गद्य में कहानी, निबन्ध, यात्रा-वृत्त और डायरी की समस्त विद्याएँ अपना अलगाव छोड़कर अपनी ‘चिंतन-क्षमता और सृजन-प्रक्रिया में समरस हो जाती है...आधुनिक समाज में गद्य से जो विविध अपेक्षाएँ की जाती हैं, वे यहाँ सब एकबारगी पूरी हो जाती हैं।’’
धुंध से उठती धुन एक ऐसे ही ‘समग्र, समरसी गद्य’ का जीवंत दस्तावेज है, निर्मल वर्मा के ‘मन की अन्तःप्रक्रियाओं’ का चलता-फिरता रिपोर्ताज, जिसमें पिछले वर्षों के दौरान लिखी डायरियों के अंश, यात्रा-वृत्त, पढ़ी हुई पुस्तकों की स्मृतियाँ और स्मृति की खिड़की से देखी दुनिया एक साथ पुनर्जीवित हो उठते हैं। एक तरफ़ जहाँ यह पुस्तक उस ‘धुंध’ को भेदने का प्रयास है, जो निर्मल वर्मा की कहानियों के बाहर छाई रहती है, वहीं दूसरी तरफ़ उस ‘धुन’ को पकड़ने की कोशिश है, जो उसके गद्य के भीतर एक अन्तर्निहित लय की तरह प्रवाहित होती है।
बरसों पहले निर्मल वर्मा के यात्रा-संस्मरण चीड़ों पर चाँदनी ने अपने प्रखर, प्रांजल गद्य से बरबस हिन्दी पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। एक तरह से उठती धुंध से उठती धुन उसका अगला चरण है, यदि कोई अंतर है तो इतना ही है कि एक में लेखक पश्चिमी का सम्मोहित, संत्रस्त रिपोर्टर था, जबकि इस पुस्तक में वह अपने ‘घर’ लौटता हुआ मुसाफ़िर। ‘सुलगती टहनी’ के अन्तिम अंश में वर्मा ने लिखा है कि : ‘‘रिल्के ने जिस एंजिल से ईष्या की थी, क्या इस दुनिया में उसका प्रतिरूप एक लेखक नहीं है, एक ख़बर देने वाला हरकारा-दोतरफ़ा दूत-जो ईश्वर की ख़बर मनुष्य को और धरती के सौन्दर्य की झलक ईश्वर को देता रहता है ?’’ हरकारे की यह ‘गुहार’ इस पुस्तक के हर पन्ने पर गूँजती सुनाई देती है।
धुंध से उठती धुन एक ऐसे ही ‘समग्र, समरसी गद्य’ का जीवंत दस्तावेज है, निर्मल वर्मा के ‘मन की अन्तःप्रक्रियाओं’ का चलता-फिरता रिपोर्ताज, जिसमें पिछले वर्षों के दौरान लिखी डायरियों के अंश, यात्रा-वृत्त, पढ़ी हुई पुस्तकों की स्मृतियाँ और स्मृति की खिड़की से देखी दुनिया एक साथ पुनर्जीवित हो उठते हैं। एक तरफ़ जहाँ यह पुस्तक उस ‘धुंध’ को भेदने का प्रयास है, जो निर्मल वर्मा की कहानियों के बाहर छाई रहती है, वहीं दूसरी तरफ़ उस ‘धुन’ को पकड़ने की कोशिश है, जो उसके गद्य के भीतर एक अन्तर्निहित लय की तरह प्रवाहित होती है।
बरसों पहले निर्मल वर्मा के यात्रा-संस्मरण चीड़ों पर चाँदनी ने अपने प्रखर, प्रांजल गद्य से बरबस हिन्दी पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। एक तरह से उठती धुंध से उठती धुन उसका अगला चरण है, यदि कोई अंतर है तो इतना ही है कि एक में लेखक पश्चिमी का सम्मोहित, संत्रस्त रिपोर्टर था, जबकि इस पुस्तक में वह अपने ‘घर’ लौटता हुआ मुसाफ़िर। ‘सुलगती टहनी’ के अन्तिम अंश में वर्मा ने लिखा है कि : ‘‘रिल्के ने जिस एंजिल से ईष्या की थी, क्या इस दुनिया में उसका प्रतिरूप एक लेखक नहीं है, एक ख़बर देने वाला हरकारा-दोतरफ़ा दूत-जो ईश्वर की ख़बर मनुष्य को और धरती के सौन्दर्य की झलक ईश्वर को देता रहता है ?’’ हरकारे की यह ‘गुहार’ इस पुस्तक के हर पन्ने पर गूँजती सुनाई देती है।
आमुख
डायरी के ये अंश पिछले बीस-बाईस वर्षों (1973-95) के दौरान अलग-अलग स्थानों में लिखे गए थे। मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि दिल्ली के बाहर जाते ही, जब मेरा बाकी लिखना छूट जाता है, अर्से से छूटी हुई डायरी शुरू हो जाती है। क्या यह एक तरह की क्षति-पूर्ति है, घर के अभाव को बेघर अनुभवों से भरने की लालसा ? कहना मुश्किल है किन्तु इन्हें परंपरागत अर्थ में ‘यात्रा-संस्मरण’ कहना भी गलत होगा। अगर ये यात्रा हैं, तो वे स्थानों की न होकर ‘मन’ की हैं, अन्त:-प्रक्रियाओं का लेखा-जोखा, जिन्हें मैंने कच्चे माल की तरह ही प्रस्तुत करना चाहा है। जो मेरा अतीत है, वह इन डायरियों का वर्तमान है इसलिए पुरानी पोथियों से उतारकर इन्हें दुबारा से टीपते हुए मेरा काल-बोध बार-बार हिचकोले खाने लगता है हम वर्तमान में अपने को दुबारा से व्यतीत कर रहे हैं, कि वर्तमान के इस क्षण में-जब मैं डायरी टीप रहा हूं-मैं एक दूसरा वर्तमान जी रहा हूँ। कभी-कभी तो मुझे गहरा अचरज होता था कि क्या यह सचमुच मेरे साथ घटा था, जिसे मैं टीप रहा हूं ?
यहाँ एक छोटा-सा स्पष्टीकरण जरूरी जान पड़ता है। इस पुस्तक में मैंने अपने दो रिपोर्ताज, ‘सिंगरौली, जहाँ कोई वापसी नहीं’ और ‘सुलगती टहनी’ भी शामिल किए हैं। इन्हें यहाँ देने का औचित्य इतना ही है कि वे मूलत: ‘निबंध विधा’ में नहीं, डायरी की तात्कालिक अंत:प्रक्रियाओं के रूप में लिखे गए थे-और उसी रूप में पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुए थे। लिखते हुए मैंने नहीं सोचा था कि अपने ढंग से वे भारतीय संस्कृति के समकालीन संकट को दो विपरीत दिशाओं से स्पर्श करेंगे। यदि प्रयाग के कुंभ मेले में भटकते हुए मुझे अपनी संस्कृति की तीन हजार वर्ष लंबी, अविरल धारा से साक्षात् हुआ, तो सिंगरौली में उस ‘इतिहास’ का साक्षी होना पड़ा, जो ‘आधुनिकता’ के नाम पर उसे इतना विकराल पैमाने पर नष्ट कर रहा है। यह आँखों देखा सत्य था, इसलिए मैंने इन्हें ‘रिपोर्ताज’ कहना ज़्यादा उचित समझा है।
अंत में शायद यह कहना भी जरूरी है, कि पुस्तक में अंकित अंत:प्रक्रियाओं का समय सीधा-सीधा कैलेण्डर की तिथियों का अनुकरण नहीं करता, हालांकि कोशिश यही रही है कि समय की अनुक्रमिक रेखा के साथ अधिक छेड़छाड़ न की जाए। डायरी हमेशा जल्दी में लिखी जाती है, उड़ते हुए अनुभवों को पूरी फड़फड़ाहट के साथ पकड़ने का प्रलोभन रहता है, अनेक वाक्य अधूरे रह जाते हैं, कई बार अंग्रेजी के शब्द घुमड़ते चले आते हैं, एक लस्तम-पस्तम रौ में बहते हुए। पांडुलिपि तैयार करते समय उसमें अनेक बार सुधार और संशोधन करना पड़ा है-लेकिन ज़्यादा नहीं। कई बार अपने हाथ रोकने पड़े हैं, कि कहीं वह धुन हाथ से न निकल जाए, जिसे बहती हुई धुंध में पकड़ा था।
यहाँ एक छोटा-सा स्पष्टीकरण जरूरी जान पड़ता है। इस पुस्तक में मैंने अपने दो रिपोर्ताज, ‘सिंगरौली, जहाँ कोई वापसी नहीं’ और ‘सुलगती टहनी’ भी शामिल किए हैं। इन्हें यहाँ देने का औचित्य इतना ही है कि वे मूलत: ‘निबंध विधा’ में नहीं, डायरी की तात्कालिक अंत:प्रक्रियाओं के रूप में लिखे गए थे-और उसी रूप में पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुए थे। लिखते हुए मैंने नहीं सोचा था कि अपने ढंग से वे भारतीय संस्कृति के समकालीन संकट को दो विपरीत दिशाओं से स्पर्श करेंगे। यदि प्रयाग के कुंभ मेले में भटकते हुए मुझे अपनी संस्कृति की तीन हजार वर्ष लंबी, अविरल धारा से साक्षात् हुआ, तो सिंगरौली में उस ‘इतिहास’ का साक्षी होना पड़ा, जो ‘आधुनिकता’ के नाम पर उसे इतना विकराल पैमाने पर नष्ट कर रहा है। यह आँखों देखा सत्य था, इसलिए मैंने इन्हें ‘रिपोर्ताज’ कहना ज़्यादा उचित समझा है।
अंत में शायद यह कहना भी जरूरी है, कि पुस्तक में अंकित अंत:प्रक्रियाओं का समय सीधा-सीधा कैलेण्डर की तिथियों का अनुकरण नहीं करता, हालांकि कोशिश यही रही है कि समय की अनुक्रमिक रेखा के साथ अधिक छेड़छाड़ न की जाए। डायरी हमेशा जल्दी में लिखी जाती है, उड़ते हुए अनुभवों को पूरी फड़फड़ाहट के साथ पकड़ने का प्रलोभन रहता है, अनेक वाक्य अधूरे रह जाते हैं, कई बार अंग्रेजी के शब्द घुमड़ते चले आते हैं, एक लस्तम-पस्तम रौ में बहते हुए। पांडुलिपि तैयार करते समय उसमें अनेक बार सुधार और संशोधन करना पड़ा है-लेकिन ज़्यादा नहीं। कई बार अपने हाथ रोकने पड़े हैं, कि कहीं वह धुन हाथ से न निकल जाए, जिसे बहती हुई धुंध में पकड़ा था।
निर्मल वर्मा
पीड़ा में पक्षी
शिमला : 12 जून, 1973
क्या संपूर्ण निराशा में लिखना संभव है ? काफ़्का आखिर तक लिखते रहे-और वे लोग भी जो मृत्यु को जानते थे। ‘‘आत्मा क्या है ?’’ किर्केगार्द ने पूछा था। ‘‘आत्मा वह है कि हम इस तरह जी सकें जैसे हम मर गए हैं, दुनिया की तरफ से मृत।’’
जब हम जवान होते हैं, हम समय के खिलाफ़ भागते हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों बूढ़े होते जाते हैं, हम ठहर जाते हैं, समय भी ठहर जाता है, सिर्फ मृत्यु भागती है, हमारी तरफ।
माल्टे, हमें कभी आकांक्षा करना नहीं छोड़ना चाहिए। मैं जानता हूँ, कोई पूर्ति नहीं है, लेकिन ऐसी आकांक्षाएँ हैं, जो आजीवन कायम रहती हैं, इसलिए तुम चाहो तो भी उनकी पूर्ति की प्रतीक्षा नहीं कर सकते।
जब हम जवान होते हैं, हम समय के खिलाफ़ भागते हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों बूढ़े होते जाते हैं, हम ठहर जाते हैं, समय भी ठहर जाता है, सिर्फ मृत्यु भागती है, हमारी तरफ।
माल्टे, हमें कभी आकांक्षा करना नहीं छोड़ना चाहिए। मैं जानता हूँ, कोई पूर्ति नहीं है, लेकिन ऐसी आकांक्षाएँ हैं, जो आजीवन कायम रहती हैं, इसलिए तुम चाहो तो भी उनकी पूर्ति की प्रतीक्षा नहीं कर सकते।
-रिल्के
अकेले रहने की एक तसल्ली है कि हमारे पास सिवा अपने के कुछ नहीं है, और मैं अपने से सिवा लिखने के-कुछ भी नहीं कर सकता।
रिल्के ने एक युवा कवि को सलाह दी थी, ‘‘रात की सबसे खामोश घड़ी में अपने से पूछो क्या लिखना अनिवार्य है ? उत्तर ‘हाँ’ में होना चाहिए, अगर तुम अकेले रह रहे हो और सिवा अपने के, कहीं और नहीं मुड़ सकते।’’
क्या बिना ईश्वर में विश्वास किए कोई संत हो सकता है ?
जिस हद तक तुम इस दुनिया में उलझे हो, उस हद तक तुम उसे खो देते हो। कलाकार दुनिया को छोड़ता है, ताकि उसे अपने कृतित्व में पा सके। तुम यथार्थ को अपने पास रखकर उसका सृजन नहीं कर सकते। तुम्हें उसके लिए मरना होगा, ताकि वह तुम्हारे लिए जीवित हो सके।
यह काफी नहीं है कि तुम इस दुनिया को एक माया की तरह अनुभव कर सको, तु्म्हें माया के यथार्थ को भी जानना होगा। वास्तव में इन दोनों सत्यों को-यथार्थ की माया और माया के यथार्थ को एक साथ और एक समय में पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तभी यह संभव हो सकेगा कि हम दुनिया के साथ पूरी तरह जुड़कर भी पूरी तरह निस्संग रह सकें।
मेरे लिए लिखना और लौटना एक चीज है। प्रतीक्षा करने से मस्तिष्क एकदम सजग हो जाता है। वह एक तरह की सीमा-रेखा है-शून्य और कुछ के बीच।
लिखना एक सक्रिय किस्म की उम्मीद है।
रिल्के ने एक युवा कवि को सलाह दी थी, ‘‘रात की सबसे खामोश घड़ी में अपने से पूछो क्या लिखना अनिवार्य है ? उत्तर ‘हाँ’ में होना चाहिए, अगर तुम अकेले रह रहे हो और सिवा अपने के, कहीं और नहीं मुड़ सकते।’’
क्या बिना ईश्वर में विश्वास किए कोई संत हो सकता है ?
जिस हद तक तुम इस दुनिया में उलझे हो, उस हद तक तुम उसे खो देते हो। कलाकार दुनिया को छोड़ता है, ताकि उसे अपने कृतित्व में पा सके। तुम यथार्थ को अपने पास रखकर उसका सृजन नहीं कर सकते। तुम्हें उसके लिए मरना होगा, ताकि वह तुम्हारे लिए जीवित हो सके।
यह काफी नहीं है कि तुम इस दुनिया को एक माया की तरह अनुभव कर सको, तु्म्हें माया के यथार्थ को भी जानना होगा। वास्तव में इन दोनों सत्यों को-यथार्थ की माया और माया के यथार्थ को एक साथ और एक समय में पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तभी यह संभव हो सकेगा कि हम दुनिया के साथ पूरी तरह जुड़कर भी पूरी तरह निस्संग रह सकें।
मेरे लिए लिखना और लौटना एक चीज है। प्रतीक्षा करने से मस्तिष्क एकदम सजग हो जाता है। वह एक तरह की सीमा-रेखा है-शून्य और कुछ के बीच।
लिखना एक सक्रिय किस्म की उम्मीद है।
-टॉमस मान
सिमोन वेल का लेखन : कर्तव्य, स्वीकार करना, पवित्रता, गरीबी का भाव, आज्ञापालन।
आज्ञा-पालन सबसे ज्यादा।
एक अच्छा उपन्यासकार अपनी सहानुभूति को बराबर-बराबर मात्रा में सब पात्रों को देता है, एक महान उपन्यासकार अपनी सहानुभूति के विरुद्ध संघर्ष करता है।
हमें पश्चिमी सभ्यता को इतिहास के संदर्भ में देखना चाहिए, क्योंकि इतिहास ने उसे पाला-पोसा है। इसके विपरीत भारतीय संस्कृति के संदर्भ में हमें इतिहास को देखना चाहिए क्योंकि उसने इतिहास को अस्वीकृत करके अपना अस्तित्व बनाया है।
इससे हमें इतिहास और संस्कृति दोनों के बारे में एक नई समझ मिल सकेगी।
मैं आन्द्रे जीद के जर्नल्स के अंतिम पृष्ठ पढ़ रहा था, जो उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले लिखे थे। ये पृष्ठ शायद उनकी डायरी में सबसे अधिक मर्मस्पर्शी हैं। देह और आत्मा के संबंध में वह जो कुछ कहते हैं-‘एक को दूसरे के बिना नहीं सोचा जा सकता’-वह ऐसा सत्य है, जिस पर मैं हमेशा विश्वास करता आया हूँ। अंतिम साँस तक जीद की तर्कशक्ति एक उज्जवल, चमकीली लौ की तरह सुलगती रही, ‘‘अपने को मुक्त करना कुछ भी नहीं है, मुक्त रहना (बीइंग फ्री) यह कठिन काम है।’’
जर्नल के इन पृष्ठों को पढ़ते समय मैं बीथोवन का रिकार्ड ‘टेम्पेस्ट’ सुन रहा था-अचानक कमरें में हवा का झोंका आया और मुझे लगा जैसे यह कोई बहुत साल बीते किसी दूसरे वसंत की हवा हो। ऐसे क्षणों में लगता है कि हम सचमुच सुखी हैं, सुखी हो सकते हैं, हम उन स्थानों में जा सकते हैं, जहाँ अभी तक नहीं गए, उन किताबों को पढ़ सकते हैं, जो अभी तक नहीं पढ़ीं, उन कहानियों को लिख सकते हैं, जो अभी तक नहीं लिखी गई।
कौन कहता है, आदमी की जिंदगी छोटी है ?
हम कितनी ही कोशिश क्यों न करें, चीज़ों के रूप के पीछे हम वास्तविकता को नहीं पकड़ सकते। इसका भयानक-सा कारण यह हो सकता है कि चीज़ों के अनुभव से अलग उनकी कोई अलग वास्तविकता नहीं है-सिर्फ उथले लोग यह कहते हैं कि चीज़ों को उनके बाहरी रूप से नहीं जाना जा सकता। दुनिया का असली रहस्य दृश्य में निहित है, अदृश्य में नहीं।
आज्ञा-पालन सबसे ज्यादा।
एक अच्छा उपन्यासकार अपनी सहानुभूति को बराबर-बराबर मात्रा में सब पात्रों को देता है, एक महान उपन्यासकार अपनी सहानुभूति के विरुद्ध संघर्ष करता है।
हमें पश्चिमी सभ्यता को इतिहास के संदर्भ में देखना चाहिए, क्योंकि इतिहास ने उसे पाला-पोसा है। इसके विपरीत भारतीय संस्कृति के संदर्भ में हमें इतिहास को देखना चाहिए क्योंकि उसने इतिहास को अस्वीकृत करके अपना अस्तित्व बनाया है।
इससे हमें इतिहास और संस्कृति दोनों के बारे में एक नई समझ मिल सकेगी।
मैं आन्द्रे जीद के जर्नल्स के अंतिम पृष्ठ पढ़ रहा था, जो उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले लिखे थे। ये पृष्ठ शायद उनकी डायरी में सबसे अधिक मर्मस्पर्शी हैं। देह और आत्मा के संबंध में वह जो कुछ कहते हैं-‘एक को दूसरे के बिना नहीं सोचा जा सकता’-वह ऐसा सत्य है, जिस पर मैं हमेशा विश्वास करता आया हूँ। अंतिम साँस तक जीद की तर्कशक्ति एक उज्जवल, चमकीली लौ की तरह सुलगती रही, ‘‘अपने को मुक्त करना कुछ भी नहीं है, मुक्त रहना (बीइंग फ्री) यह कठिन काम है।’’
जर्नल के इन पृष्ठों को पढ़ते समय मैं बीथोवन का रिकार्ड ‘टेम्पेस्ट’ सुन रहा था-अचानक कमरें में हवा का झोंका आया और मुझे लगा जैसे यह कोई बहुत साल बीते किसी दूसरे वसंत की हवा हो। ऐसे क्षणों में लगता है कि हम सचमुच सुखी हैं, सुखी हो सकते हैं, हम उन स्थानों में जा सकते हैं, जहाँ अभी तक नहीं गए, उन किताबों को पढ़ सकते हैं, जो अभी तक नहीं पढ़ीं, उन कहानियों को लिख सकते हैं, जो अभी तक नहीं लिखी गई।
कौन कहता है, आदमी की जिंदगी छोटी है ?
हम कितनी ही कोशिश क्यों न करें, चीज़ों के रूप के पीछे हम वास्तविकता को नहीं पकड़ सकते। इसका भयानक-सा कारण यह हो सकता है कि चीज़ों के अनुभव से अलग उनकी कोई अलग वास्तविकता नहीं है-सिर्फ उथले लोग यह कहते हैं कि चीज़ों को उनके बाहरी रूप से नहीं जाना जा सकता। दुनिया का असली रहस्य दृश्य में निहित है, अदृश्य में नहीं।
-आस्कर वाइल्ड
साहित्य हमें पानी नहीं देता, वह सिर्फ़ हमें अपनी प्यास का बोध कराता है। जब तुम स्वप्न में पानी पीते हो, तो जागने पर सहसा एहसास होता है कि तुम सचमुच कितने प्यासे थे।
मनुष्य की कमज़ोरियों में हमेशा एक ‘कॉमिक’ तत्व छिपा रहता है। नाटक में जिसे हम ट्रेजेडी कहते हैं, वह और कुछ नहीं, उन तत्वों की मंच पर तीव्रतम अभिव्यक्ति है, जिन पर हम वास्तविक जिंदगी में हँस सकते हैं। क्या यह कारण नहीं है, कि एक महान् अभिनेता हमेशा ट्रेजिक होता है, भले ही वह ‘कॉमिक’ भूमिका क्यों न अदा करे क्योंकि वह हमेशा सीमा का उल्लंघन करता है, जीवन के ‘सुखद संतुलन’ को भंग करता है।
कुछ संबंधों से हम बाहर नहीं निकल सकते-कोशिश करें, तो निकलने की कोशिश में माँस के लोथड़े बाहर आ जाएँगे, खून में टिपटिपाते हुए।
जुदाई का हर निर्णय संपूर्ण और अंतिम होना चाहिए; पीछे छोड़े हुए सब स्मृतिचिह्नों को मिटा देना चाहिए, और पुलों को नष्ट कर देना चाहिए, किसी भी तरह की वापसी को असंभव बनाने के लिए।
यह ख़याल ही कितनी सांत्वना देता है कि हर दिन, वह चाहे कितना लंबा, असह्य क्यों न हो, उसका अंत शाम में होगा, एक शीतल-से झुटपुटे में। मैं कमरे से बाहर जाऊँगा, स्मृतियों की छत से बाहर, गर्मी के खुले आकाश में, तारों के नीचे, बिना किसी आशा और प्रतीक्षा के।
हर पीड़ायुक्त निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए हमें उसे दैनिक जीवन का स्वाभाविक अंग बनाना होगा। तभी हम उसे भूल सकते हैं, जिसे हमने खो दिया है।
यह थकान-इसके नीचे लेट जाना चाहिए, इसकी ठंडी घनी छाया के नीचे जहाँ विरक्ति की अलमस्त लहर घेर लेती है...पीड़ा, इच्छा, उम्मीद का वह पता कहाँ गया, क्या शून्यता से टकराकर झर गया...या वह अब भी वहीं है, निश्चल, शांत, आँखों से ओझल ?
एक ज़िंदगी जो बीच में कट जाती है अपने में संपूर्ण है। उसके आगे का समय उसके साथ ही मर जाता है जैसे उम्र की रेखा-वह चाहे कितनी लंबी क्यों न हो-मृत हथेली पर मुरझाने लगती है। क्या रिश्तों के साथ भी ऐसा होता है जो बीच में टूट जाते हैं ? हम विगत के बारे में सोचते हुए पछताते हैं कि उसे बचाया जा सकता था, बिना यह जाने कि स्मृतियाँ उसे नहीं बचा सकतीं, जो बीत गया है। मरे हुए रिश्ते पर वे उसी तरह रेंगने लगती हैं जैसे शव पर च्यूँटियाँ। दो चरम बिंदुओं के बीच झूलता हुआ आदमी। क्या उन्हें (बिंदुओं को) नाम दिया जा सकता है ? दोनों के बीच जो है, वह सत्य नहीं पीड़ा है। वह एक अर्धसत्य और दूसरे अर्धसत्य के बीच पेंडुलम की तरह डोलता है, उन्हें संपूर्ण पाने के लिए, लेकिन अपनी गति में-जो उसकी आदिम अवस्था है-हमेशा अपूर्ण रहता है।
मनुष्य की कमज़ोरियों में हमेशा एक ‘कॉमिक’ तत्व छिपा रहता है। नाटक में जिसे हम ट्रेजेडी कहते हैं, वह और कुछ नहीं, उन तत्वों की मंच पर तीव्रतम अभिव्यक्ति है, जिन पर हम वास्तविक जिंदगी में हँस सकते हैं। क्या यह कारण नहीं है, कि एक महान् अभिनेता हमेशा ट्रेजिक होता है, भले ही वह ‘कॉमिक’ भूमिका क्यों न अदा करे क्योंकि वह हमेशा सीमा का उल्लंघन करता है, जीवन के ‘सुखद संतुलन’ को भंग करता है।
कुछ संबंधों से हम बाहर नहीं निकल सकते-कोशिश करें, तो निकलने की कोशिश में माँस के लोथड़े बाहर आ जाएँगे, खून में टिपटिपाते हुए।
जुदाई का हर निर्णय संपूर्ण और अंतिम होना चाहिए; पीछे छोड़े हुए सब स्मृतिचिह्नों को मिटा देना चाहिए, और पुलों को नष्ट कर देना चाहिए, किसी भी तरह की वापसी को असंभव बनाने के लिए।
यह ख़याल ही कितनी सांत्वना देता है कि हर दिन, वह चाहे कितना लंबा, असह्य क्यों न हो, उसका अंत शाम में होगा, एक शीतल-से झुटपुटे में। मैं कमरे से बाहर जाऊँगा, स्मृतियों की छत से बाहर, गर्मी के खुले आकाश में, तारों के नीचे, बिना किसी आशा और प्रतीक्षा के।
हर पीड़ायुक्त निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए हमें उसे दैनिक जीवन का स्वाभाविक अंग बनाना होगा। तभी हम उसे भूल सकते हैं, जिसे हमने खो दिया है।
यह थकान-इसके नीचे लेट जाना चाहिए, इसकी ठंडी घनी छाया के नीचे जहाँ विरक्ति की अलमस्त लहर घेर लेती है...पीड़ा, इच्छा, उम्मीद का वह पता कहाँ गया, क्या शून्यता से टकराकर झर गया...या वह अब भी वहीं है, निश्चल, शांत, आँखों से ओझल ?
एक ज़िंदगी जो बीच में कट जाती है अपने में संपूर्ण है। उसके आगे का समय उसके साथ ही मर जाता है जैसे उम्र की रेखा-वह चाहे कितनी लंबी क्यों न हो-मृत हथेली पर मुरझाने लगती है। क्या रिश्तों के साथ भी ऐसा होता है जो बीच में टूट जाते हैं ? हम विगत के बारे में सोचते हुए पछताते हैं कि उसे बचाया जा सकता था, बिना यह जाने कि स्मृतियाँ उसे नहीं बचा सकतीं, जो बीत गया है। मरे हुए रिश्ते पर वे उसी तरह रेंगने लगती हैं जैसे शव पर च्यूँटियाँ। दो चरम बिंदुओं के बीच झूलता हुआ आदमी। क्या उन्हें (बिंदुओं को) नाम दिया जा सकता है ? दोनों के बीच जो है, वह सत्य नहीं पीड़ा है। वह एक अर्धसत्य और दूसरे अर्धसत्य के बीच पेंडुलम की तरह डोलता है, उन्हें संपूर्ण पाने के लिए, लेकिन अपनी गति में-जो उसकी आदिम अवस्था है-हमेशा अपूर्ण रहता है।
शिमला इंस्टीट्यूट, जून 1973
दिन भर बारिश होती रही।
परसों राम, बहिन और उसके बच्चों के साथ कामना देवी के मंदिर गए। बदली का दिन था, लेकिन बीच-बीच में सूरज निकल आता था। पहाड़ियों के विस्तीर्ण फैलाव को देखा, जिन पर शिमले का हिल-स्टेशन टिका है। उनके साथ बोलते, हँसते हुए मैं सब कुछ भूल गया।
शाम को जब वे चले गए, मैं कमरे में बैठा हाना अरेंड्ट की पुस्तक हिंसा पर (On Violence) पढ़ता रहा।
अब बारिश और अँधेरा है। मैं टेबल-लैंप जलाते हुए डरता हूँ-उस आत्मीय अँधेरे को तोड़ना नहीं चाहता जो दिन भर मेरे कमरे में मेरे भीतर, मेरे साथ, जमा होता गया है।
मैं हाइनरिख ब्योल का उपन्यास पढ़ रहा हूं। बहुत ‘सच्ची’ किताब है। इसके अलावा कोई दूसरा विशेषण याद नहीं आता। अपने निजी स्वर में बहुत प्रेरणादायक भी। बार-बार उसे पढ़ते हुए मुझे अपना वह ‘आत्म-जीवनी’ सरीखा उपन्यास याद आता रहा, जो प्राग में शुरू किया था और जो अपने अधूरेपन में मुझे आज भी त्रस्त करता है।
क्या मैं एक ही समय में ‘सच्चा’ और कलात्मक दोनों हो सकता हूँ ? क्या हम पूरी ईमानदारी से जीवन के कच्चे माल को एक कलाकृति में परिणत कर सकते हैं ? क्या कला जीवन के झूठों को अपने में समो सकती है, काले जहर की तरह, जिसका निशान शिव के नीलकंठ की तरह ही-उसकी सही पहचान बन जाता है ?
जीवन में असफल होने का एक फायदा यह है कि मेरे पास अपने होने के अलावा और कुछ नहीं है और जब मेरे पास सिर्फ़ ‘मैं’ हूं तो मैं उसे सिर्फ़ लिखने के लिए ही इस्तेमाल कर सकता हूँ कुछ वैसे ही जैसे अलिफ़-लैला के एक किस्से में एक आदमी शैतान से छुटकारा पाने के लिए उसे किसी न किसी काम में लगाए रहता है। वह अभिशाप भी है और वरदान भी।
परसों राम, बहिन और उसके बच्चों के साथ कामना देवी के मंदिर गए। बदली का दिन था, लेकिन बीच-बीच में सूरज निकल आता था। पहाड़ियों के विस्तीर्ण फैलाव को देखा, जिन पर शिमले का हिल-स्टेशन टिका है। उनके साथ बोलते, हँसते हुए मैं सब कुछ भूल गया।
शाम को जब वे चले गए, मैं कमरे में बैठा हाना अरेंड्ट की पुस्तक हिंसा पर (On Violence) पढ़ता रहा।
अब बारिश और अँधेरा है। मैं टेबल-लैंप जलाते हुए डरता हूँ-उस आत्मीय अँधेरे को तोड़ना नहीं चाहता जो दिन भर मेरे कमरे में मेरे भीतर, मेरे साथ, जमा होता गया है।
मैं हाइनरिख ब्योल का उपन्यास पढ़ रहा हूं। बहुत ‘सच्ची’ किताब है। इसके अलावा कोई दूसरा विशेषण याद नहीं आता। अपने निजी स्वर में बहुत प्रेरणादायक भी। बार-बार उसे पढ़ते हुए मुझे अपना वह ‘आत्म-जीवनी’ सरीखा उपन्यास याद आता रहा, जो प्राग में शुरू किया था और जो अपने अधूरेपन में मुझे आज भी त्रस्त करता है।
क्या मैं एक ही समय में ‘सच्चा’ और कलात्मक दोनों हो सकता हूँ ? क्या हम पूरी ईमानदारी से जीवन के कच्चे माल को एक कलाकृति में परिणत कर सकते हैं ? क्या कला जीवन के झूठों को अपने में समो सकती है, काले जहर की तरह, जिसका निशान शिव के नीलकंठ की तरह ही-उसकी सही पहचान बन जाता है ?
जीवन में असफल होने का एक फायदा यह है कि मेरे पास अपने होने के अलावा और कुछ नहीं है और जब मेरे पास सिर्फ़ ‘मैं’ हूं तो मैं उसे सिर्फ़ लिखने के लिए ही इस्तेमाल कर सकता हूँ कुछ वैसे ही जैसे अलिफ़-लैला के एक किस्से में एक आदमी शैतान से छुटकारा पाने के लिए उसे किसी न किसी काम में लगाए रहता है। वह अभिशाप भी है और वरदान भी।
13 नवंबर, 1974
आज दुपहर फागू चला आया, शिमला की दीवाली से दूर जाने की इच्छा थी-और अपने से भी दूर जाने की...
यह जगह शिमला से पंद्रह मील की दूरी पर है-बस में सिर्फ़ एक घंटा लगता है, लेकिन इतने कम समय में दुनिया के दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। यह एक छोटा-सा पहाड़ी गाँव है, थियोग और कुफ्री के बीच पहाड़ों से घिरा हुआ। बहुत पहले यहाँ राम जमीन खरीदना चाहते थे। घूमते हुए मैं सोचने लगा क्या यहाँ कोई रह सकता है ? पहले-पहल तो मुक्ति का उल्लास होता है, किंतु क्या कोई हर दिन इतनी वीरानी सह सकता है ?
मैं एक रेस्ट हाउस में ठहरा हूँ-जो एक उठान पर स्थित है। रेस्ट हाउस के सारे कमरे खाली पड़े हैं। अकेला एक मैं हूँ। यह शायद मेरी नियति है-इंस्टीट्यूट के अकेलेपन से बचकर यहां के अकेलेपन में आना। मैं यह भी भूल गया हूँ कि मुझे अब अकेलेपन में कैसा लगता है। अब मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं मानो वह मेरे ‘होने’ का ही अंग है, एक छाया जो हर जगह मेरे पीछे चलती है, एक अवसन्न छाया, आत्मा से जुड़ी हुई।
‘‘तुम उस दुनिया में रहते हो, जो तुमने बनाई है।’’ यह वाक्य मैंने कल पढ़ा था।
पहाड़ी रेस्ट हाउस की रातें। कमरों की धुँधुआती रोशनियाँ। बाहर हवा चलती है। नीचे मोटर-रोड से बसों की गड़गड़ाहट पहाड़ियों में गूँजती हुई आती है। नीचे घाटी में दीवाली के पटाखे, जैसे अँधेरे में कोई बंदूक से फायरिंग कर रहा हो। दूर पहाड़ों पर धूप का एक टुकड़ा-सूरज का मलिन-सा धब्बा दो अँधेरों के बीच तेजी से सिकुड़ता हुआ, मेरे देखते-देखते वह हवा में घुल जाता है, एक अचानक मृत्यु की तरह, कुछ भी बचा नहीं रहता।
यह एक स्वप्न नगरी है...पत्थर के मकान, लुटी-पिटी दुकानों के खँडहर, एक ‘अंग्रेजी शराब’ की दुकान मोटर-रोड पर और उसके नीचे, एक गली में देसी ठर्रे का खोखा, जिसके इर्द-गिर्द शराब में धुत्त कुछ अनिश्चित से चुंधियाई आँखों से मुझे ताकते पहाड़ी, उनके हलके लड़खड़ाते पैर....
मैं पहाड़ी की चोटी पर गया, जहाँ देवी का एक मंदिर था, लेकिन मूर्ति की जगह सिर्फ एक शिला-खंड था; सामने पेड़ पर हवा में फड़फड़ाती रंग-बिरंगी झंडियाँ।
यह जगह शिमला से पंद्रह मील की दूरी पर है-बस में सिर्फ़ एक घंटा लगता है, लेकिन इतने कम समय में दुनिया के दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। यह एक छोटा-सा पहाड़ी गाँव है, थियोग और कुफ्री के बीच पहाड़ों से घिरा हुआ। बहुत पहले यहाँ राम जमीन खरीदना चाहते थे। घूमते हुए मैं सोचने लगा क्या यहाँ कोई रह सकता है ? पहले-पहल तो मुक्ति का उल्लास होता है, किंतु क्या कोई हर दिन इतनी वीरानी सह सकता है ?
मैं एक रेस्ट हाउस में ठहरा हूँ-जो एक उठान पर स्थित है। रेस्ट हाउस के सारे कमरे खाली पड़े हैं। अकेला एक मैं हूँ। यह शायद मेरी नियति है-इंस्टीट्यूट के अकेलेपन से बचकर यहां के अकेलेपन में आना। मैं यह भी भूल गया हूँ कि मुझे अब अकेलेपन में कैसा लगता है। अब मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं मानो वह मेरे ‘होने’ का ही अंग है, एक छाया जो हर जगह मेरे पीछे चलती है, एक अवसन्न छाया, आत्मा से जुड़ी हुई।
‘‘तुम उस दुनिया में रहते हो, जो तुमने बनाई है।’’ यह वाक्य मैंने कल पढ़ा था।
पहाड़ी रेस्ट हाउस की रातें। कमरों की धुँधुआती रोशनियाँ। बाहर हवा चलती है। नीचे मोटर-रोड से बसों की गड़गड़ाहट पहाड़ियों में गूँजती हुई आती है। नीचे घाटी में दीवाली के पटाखे, जैसे अँधेरे में कोई बंदूक से फायरिंग कर रहा हो। दूर पहाड़ों पर धूप का एक टुकड़ा-सूरज का मलिन-सा धब्बा दो अँधेरों के बीच तेजी से सिकुड़ता हुआ, मेरे देखते-देखते वह हवा में घुल जाता है, एक अचानक मृत्यु की तरह, कुछ भी बचा नहीं रहता।
यह एक स्वप्न नगरी है...पत्थर के मकान, लुटी-पिटी दुकानों के खँडहर, एक ‘अंग्रेजी शराब’ की दुकान मोटर-रोड पर और उसके नीचे, एक गली में देसी ठर्रे का खोखा, जिसके इर्द-गिर्द शराब में धुत्त कुछ अनिश्चित से चुंधियाई आँखों से मुझे ताकते पहाड़ी, उनके हलके लड़खड़ाते पैर....
मैं पहाड़ी की चोटी पर गया, जहाँ देवी का एक मंदिर था, लेकिन मूर्ति की जगह सिर्फ एक शिला-खंड था; सामने पेड़ पर हवा में फड़फड़ाती रंग-बिरंगी झंडियाँ।
2 दिसंबर, 1974
दुपहर के चार बजे;
पहाड़ी ट्रेन की सीटी भी-सूरज को काटती हुई-यही कहती है।
मैं दिल को सुनता हूँ उसके हृदयहीन पंखों को,
क्या कोई पक्षी पीड़ा में है ?
मैं यह भी नहीं कह सकता, मत हिलो,
ठहरो,
पीड़ा को थम जाने दो,
लेकिन वे समझते नहीं,
न दिल,
न उसके भीतर हिलता हुआ पक्षी
दुपहर के चार बजे।
अब कुछ भी नहीं है, उतना भी नहीं, जिसमें अपने न होने को समर्पित किया जा सके। जब कुछ भी नहीं रहता, तो शून्यता का स्वच्छ बोध भी, जो हमेशा भीतर रहता था, हमारा साथ छोड़ देता है।
लेकिन जब कुछ भी नहीं रहता, तो मैं कुछ भी हो सकता हूं-एक वृक्ष, एक पत्ता, एक पत्थर। और यह खयाल ही कि हम ‘कुछ नहीं’ से भी कम हो सकते हैं, मृत से अधिक मृत-एक गहरी सांत्वना देता है, जैसे बचपन में, बीमारी की रात, माँ का हाथ अँधेरे में सहलाता है....
जिस दिन मैं अपने अकेलेपन का सामना कर पाऊँगा-बिना किसी आशा के-ठीक तब मेरे लिए आशा होगी, कि मैं अकेलेपन में जी सकूँ।
मेरे कोई मित्र नहीं है, मुझे अपने साथ अकेले रहना होगा
लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी कला में ईश्वर दूसरों से अधिक मेरे निकट है। मैं बिना किसी भय के उसके साथ रह सकता हूँ। हर बार मैंने उसे पहचाना है, समझा है। न मुझे अपने संगीत के बारे में कोई चिंता है, उस पर कभी किसी अनिष्ट की छाया नहीं पड़ सकती। जो उसे समझेंगे, हमेशा के लिए उन तमाम दुखों से छुटकारा पा लेंगे, जिन्हें दूसरे लोग आजीवन अपने साथ घसीटते हैं।
पहाड़ी ट्रेन की सीटी भी-सूरज को काटती हुई-यही कहती है।
मैं दिल को सुनता हूँ उसके हृदयहीन पंखों को,
क्या कोई पक्षी पीड़ा में है ?
मैं यह भी नहीं कह सकता, मत हिलो,
ठहरो,
पीड़ा को थम जाने दो,
लेकिन वे समझते नहीं,
न दिल,
न उसके भीतर हिलता हुआ पक्षी
दुपहर के चार बजे।
अब कुछ भी नहीं है, उतना भी नहीं, जिसमें अपने न होने को समर्पित किया जा सके। जब कुछ भी नहीं रहता, तो शून्यता का स्वच्छ बोध भी, जो हमेशा भीतर रहता था, हमारा साथ छोड़ देता है।
लेकिन जब कुछ भी नहीं रहता, तो मैं कुछ भी हो सकता हूं-एक वृक्ष, एक पत्ता, एक पत्थर। और यह खयाल ही कि हम ‘कुछ नहीं’ से भी कम हो सकते हैं, मृत से अधिक मृत-एक गहरी सांत्वना देता है, जैसे बचपन में, बीमारी की रात, माँ का हाथ अँधेरे में सहलाता है....
जिस दिन मैं अपने अकेलेपन का सामना कर पाऊँगा-बिना किसी आशा के-ठीक तब मेरे लिए आशा होगी, कि मैं अकेलेपन में जी सकूँ।
मेरे कोई मित्र नहीं है, मुझे अपने साथ अकेले रहना होगा
लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी कला में ईश्वर दूसरों से अधिक मेरे निकट है। मैं बिना किसी भय के उसके साथ रह सकता हूँ। हर बार मैंने उसे पहचाना है, समझा है। न मुझे अपने संगीत के बारे में कोई चिंता है, उस पर कभी किसी अनिष्ट की छाया नहीं पड़ सकती। जो उसे समझेंगे, हमेशा के लिए उन तमाम दुखों से छुटकारा पा लेंगे, जिन्हें दूसरे लोग आजीवन अपने साथ घसीटते हैं।
-बीथोवन
बर्फ़ पर दो छायाएँ
मुक्तेश्वर से आयोवा तक : 1975-77
ऐसी रातें हैं, जब हवा थम जाती है। सब कुछ निस्तब्ध हो जाता है। मैं खिड़की के बाहर देखता हूँ, अँधेरे में वृक्ष बिलकुल निश्चल दिखाई देते हैं। मुझे टॉलस्टॉय की याद आती है, जो बीतते हुए क्षण में ‘शाश्वत’ निश्चलता के पीछे गति, आत्मा को प्रतिबिंबित करती देह और देह के परदे पर झलकती आत्मा को अपनी कृतियों के विराट झरोखे से झलकाते थे।
एक ड्राइंग मास्टर मुझसे मिलने आए। वह पिछले सत्रह वर्षों से मुक्तेश्वर के लोकल स्कूल में पढ़ाते हैं। उनकी पत्नी अल्मोड़ा में अध्यापिका है।
हम नसबंदी की चर्चा करते रहे। अधिकांश प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की नसबंदी की जा रही है। वे कूर्मांचल के सुदूर गाँवों से मुक्तेश्वर में ‘ऑपरेशन’ कराने आते हैं। ड्राइंग मास्टर निस्संतान हैं, इसलिए उनको कोई झमेला नहीं।
उन्होंने बताया कि वह कुमाऊँ प्रदेश की लोक-चित्रकला की परंपरा पर पीएच.डी. थीसिस लिखना चाहते हैं। मैंने उसके बारे में उत्सुकता जताई तो उन्होंने अपनी थीसिस की रुपरेखा दिखाई, जो काफी विस्तार से बनाई गई थी।
एक ड्राइंग मास्टर मुझसे मिलने आए। वह पिछले सत्रह वर्षों से मुक्तेश्वर के लोकल स्कूल में पढ़ाते हैं। उनकी पत्नी अल्मोड़ा में अध्यापिका है।
हम नसबंदी की चर्चा करते रहे। अधिकांश प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की नसबंदी की जा रही है। वे कूर्मांचल के सुदूर गाँवों से मुक्तेश्वर में ‘ऑपरेशन’ कराने आते हैं। ड्राइंग मास्टर निस्संतान हैं, इसलिए उनको कोई झमेला नहीं।
उन्होंने बताया कि वह कुमाऊँ प्रदेश की लोक-चित्रकला की परंपरा पर पीएच.डी. थीसिस लिखना चाहते हैं। मैंने उसके बारे में उत्सुकता जताई तो उन्होंने अपनी थीसिस की रुपरेखा दिखाई, जो काफी विस्तार से बनाई गई थी।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book