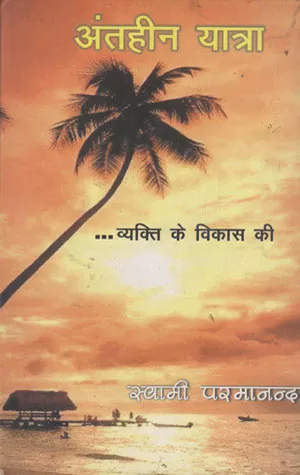|
धर्म एवं दर्शन >> अंतहीन यात्रा अंतहीन यात्रास्वामी परमानन्द
|
349 पाठक हैं |
||||||
इसमें व्यक्ति के विकास की अंतहीन यात्रा का वर्णन किया गया है.....
Anthin Yatra a hindi book by Swami Parmanand - अंतहीन यात्रा - स्वामी परमानन्द
प्रस्तुत है पुस्तक के कुछ अंश
इस अनन्त यात्रा पर हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमारे मार्गदर्शन कर सके तथा उत्साह एवं धैर्य की ज्वाला को प्रज्वलित रखे। इस पुस्तक के माध्यम से अब यह प्रबुद्ध पाठकों के लिए उपलब्ध हैं।
S.W.OAK.
Additional Secrettary MOF
Additional Secrettary MOF
स्वामी परमानन्द जी ने साधना पद्धति के सिद्धान्तों को बहुत ही वैज्ञानिक रूप से अपने शिष्यों को सिखाया है तथा अपनी लेखनी से उसको उसी तरह प्रभावपूर्ण तरीके से लिख भी डाला है। एस.सी.मित्तल पूर्व चेयरमैन,स्टाफ सलेक्शन कमीशन ध्यान योग के पथ पर जानेवाले व्यक्तियों के लिए यह अत्यन्त ही पढ़ने योग्य पुस्तक है। यह पुस्तक उन सभी मार्गों पर पूर्ण प्रकाश डालती है जिनसे, एक व्यक्ति ध्यान योग के मार्गों से होकर गुजरता है।
आनन्द के श्रीवास्तव
पूर्व चैयरमैन शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड
पूर्व चैयरमैन शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड
स्वामी परमानन्द जी के साधना सिद्धान्तों का यह संचयन आध्यात्मिक पुष्प के खुशबूदार गुलदस्ते की तरह है। इस पुस्तक (अन्तहीन यात्रा) के अन्त तक पहुँचते-पहुँचते एक रहस्य की तरह स्वामी जी हमारी उंगलियाँ पकड़कर हमारा पथ प्रदर्शन करने लगते हैं।
मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होता है। क्योंकि उसमें सोचने, समझने और विचार करने की शक्ति है। जैसी सोच और विचार होते हैं वैसी ही अभिव्यक्ति भी होती है। रोज़ाना के क्रियाकलाप पर उसका प्रभाव रहता है। परिवारजनों, मित्रों और कार्यस्थल पर वैसा ही व्यवहार परिलक्षित होता रहता है। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति की सोच और विचार अलग-अलग होते हैं, कभी दो प्राणी एक जैसे नहीं होते। मनुष्य में इसी विभिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति के विकास की यात्रा अलग-अलग होती है। इस यात्रा का अन्त तभी होता है, जब मनुष्य जीवन-मरण के क्रम से मुक्त होकर ब्रह्मलीन हो जाता है। हम सभी की यात्रा ऐसे ही समाप्त होनी है, कब होगी पता नहीं। मनुष्य योनि में आ गए हैं, तो विकास करते ही रहेंगे और कभी-न-कभी, कुछ जन्मों के बाद मुक्त होंगे ही।
जीवन को या स्वयं को समझने के लिए हमारे समाज में युगों-युगों से चितंन होता रहा है। बहुत से ऋषि, मुनियों, दार्शनिकों और चिंतकों ने बहुत-सी पुस्तकें लिखी हैं। हमारी आध्यात्मिक विचारधारा और आध्यात्मिक यात्रा ही हमें विश्व में एक विशेष स्थान प्रदान करती है।
स्वामी परमानन्द जी द्वारा लिखी यह पुस्तक कई तरह से भिन्न है। पहले तो यह स्वयं के अनुभवों पर आधारित है। वे अनुभव हिमालय की गुफा में बैठकर या दूर-दराज के इलाकों में कहीं अलग-थलग कुछ चुने हुए प्रशंसक शिष्यों के बीच के अनुभव नहीं हैं बल्कि भीड़ भरी गलियों, मुहल्लों और सुख-दुख से सनी हुई सामान्य लोगों की बातों के बीच से उत्पन्न अनुभव हैं। उन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त ज्ञान, सामान्य लोगों से मिली जानकारी, गुरुओं और महर्षि महेश योगी जैसे विचारकों के सान्निध्य से प्राप्त समझ से उभरे विश्लेषण शक्ति का उपोयग करके, क्लिष्ट विषयों पर सरलता से विवेचना की है।
हमारे समाज में विचारो में बड़ा द्वन्द्व चलता रहता है। राम बड़े हैं कि कृष्ण। राम और रावण का क्या सम्बन्ध है, क्या कबीर, बुद्ध, महावीर की विचारधाराएँ अलग-अलग हैं ? क्या फर्क है इनमें ? रावण को उसके पाण्डित्य के लिए मान दिया जाए या सीता को चुरा कर राम से युद्ध करने के लिए अपमान। पुनर्जन्म होता है कि नहीं, योग तो कई प्रकार के हैं, प्रचारक या गुरु भी कई हैं, किसे मानें किसे न मानें। कर्मयोगी बनूँ, भक्ति करूँ, हठ योग बनूँ या राजयोग को मानूँ। जीवन में लड़ाई ही लड़ाई है, द्वन्द्व ही द्वन्द्व है। हमारे लिए क्या ठीक है, कैसे चयन करें।
स्वामी परमानन्द जी के लेखों और पत्रों के इस संकलन में बड़ी सरलता से इन प्रश्नों के उत्तर दिये गये हैं, इस तरह कि, जो एक साधारण व्यक्ति के समझ मे आयें।
योग का क्या अर्थ है, शरीर क्यों है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, शरीर को आधार मानकर क्या करना है, कहाँ पहुँचना है। इन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर सरल भाषा में दिया गया है।
मैं विशेष रूप से ‘राम महामन्त्र क्यों ? और ‘मैं कृ़ष्ण का भक्त नहीं हूँ’ जैसे रोचक लेखों का उल्लेख करूँगा। इन लेखों में अत्यन्त सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। भारतीय मनीषियों का सम्यक् जीवन का दृष्टिकोण इतनी अच्छी तरह से बताया गया है जो मैंने कहीं नहीं देखा। कहा है : ‘वैदिक ऋषियों में सभी पत्नी और परिवारयुक्त थे। बुद्ध और महावीर भी विवाहित थे, तथा बुद्ध के संन्यास पूर्व एक पुत्र और महावीर के एक पुत्री थी। गृहस्थ जीवन तथा भौतिक सुख-समृद्धि का प्रयास भी वांछनीय है, पर यही अन्त नहीं है। इसके आगे भी बहुत कुछ पाने को है। जिसने सांसारिक वैभव अर्जित ही नहीं किया, उसका वैभव परित्याग या संसार से वैराग्य की बात करना विरक्ति नहीं मात्र सांत्वना है, मन समझावा। अनासक्ति का आधार पूर्ण तृप्ति होना चाहिए, न कि प्राप्त करने की अक्षमता। जब तक सांसारिक वैभव अर्जित नहीं किया जाता, तब तक यह पता नहीं चलेगा, कि वैभव से तृप्ति नहीं मिलती। कामना तो दुष्पूर है। दूसरों से सुनकर वैभव को नकारना निकम्मापन ही होगा और मन में सदैव उसके लिए रस बना रहेगा।’’
इसी तरह ‘‘अब किसी व्यक्ति की एक उँगली, क्या शरीर की भक्त हो सकती है। जो उसी का भाग है, अंश है, उसके समर्पण का क्या अर्थ है। इसीलिए मैं कृष्ण का भक्त नहीं हूँ।’’
‘‘पुनर्जन्म व्यवस्था’ पर अपने एक शिष्य को लिखे पत्र में स्वामी परमानन्द जी ने साफ कर दिया है, ‘‘मनुष्य एक यात्रा का अन्तिम पड़ाव है, जहाँ से दूसरी यात्रा शुरू होती है। अनन्त की, ब्रह्मत्व की यात्रा, मोक्ष की, निर्वाण की यात्रा। यह यात्रा यदि शुरू नहीं हो पाती तो मनुष्य जन्म मरण के एक दुष्चक में घूमता रहता है।’’
संस्कार क्या हैं एक जन्म से दूसरे जन्म में किस तरह से हस्तान्तरित होते हैं और कब विगलित हो जाते हैं बहुत सरल तरीके से बताया है।
‘‘पंचभौतिक शरीर और संस्कार आवेष्टित मन मिलकर एक व्यक्ति का निर्माण करते हैं और जीवन-यात्रा प्रारम्भ हो जाती है। यह समझ लें कि ‘संस्कार’ क्या है ? और इनका क्या महत्त्व है ? मानसिक वाचिक या शारीरिक प्रत्येक कर्म का कुछ कर्मफल होता है औश्र प्रत्येक कर्मफल मन पर एक संस्कार छोड़ जाता है। यह संस्कार स्मृति का ही अति सूक्ष्म रूप है। संस्कार ही भावी इच्छा या कामना का बीज होता है। कामना या इच्छा से विचार उत्पन्न होता है और विचार कर्म में फलित होता है। इस प्रकार संस्कार-इच्छा-विचार-कर्म-कर्फफल-संस्कार का चक्र अबाध गति से चलता रहता है।....साधना द्वारा संस्कार समूह का विगलन और मन का निर्मलन होते-होते एक दिन योग सिद्ध और संसिद्ध होकर अचानक शून्य में वह छलाँग लग जाती है-या कहें वहाँ विस्फोट हो जाता है जब व्यक्ति का व्यक्तित्व विलीन हो जाता है और वह विराट से एकाकार होकर स्वयं ‘ब्रह्म’ हो जाता है।’’
इन रोचक विषयों पर व्याख्या के बाद ध्यान योग और साधना को इतनी सरलता से समझाया गया कि लगता है, जैसे बातचीत हो रही हो। विलक्षण वाक्य है : ‘‘योग साधना का उद्देश्य है, इन संस्कार ग्रन्थियों का विगलन, नए संस्कार ग्रन्थियों के निर्माण को रोकना और जीवन त्रिभुज को संस्कारों से अलग कर मूल स्थिति में ले आना।’’ फिर राजयोग किस तरह एक गृहस्थ को जीवन के सभी कार्य करने के साथ-साथ आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर करती है, सहज तरीके से बताया गया है। देखिए कितना सरल है : ‘‘मन को विचार से निर्विचार में ले जाने अर्थात विचार को भीतर मोड़कर उसके उद्गगम तक ले जाने की क्रिया को ही ध्यान कहते हैं। इसीलिए यह प्रक्रिया ध्यान योग कहलाती है। ध्यान योग में प्रक्रिया को एक बार समझ लेने पर रोज-रोज किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती। सारी प्रगति स्वतः चालित होती है। मन पर खान-पान, रहन-सहन, तथा सोने-जागने के समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आधुनिक जीवन-पद्धति के हर वर्ग के अनुकूल पड़ता है। किसी भी स्थिति में मन विचार करता ही रहता है। अतः ध्यान वर्ग के अनुकूल पड़ता है। किसी भी स्थिति में मन विचार करता ही रहता है। अतः ध्यान योग की साधना के लिए किसी विशिष्ट स्थान या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं। आप बस में, ट्रेन में या शिप या प्लेन में कहीं भी ध्यान कर सकते हैं। आपको केवल आराम से सुखद आसन में बैठना होता है, वह चाहे कुशा-आसन हो या आरामकुर्सी, तख्त हो या वायुयान की सीट हर जगह ध्यान हो सकता है। इसीलिए यह अधिकार के साथ कहा जा सकता है, कि गृहस्थों तथा आधुनिक जीवन-पद्धति में ध्यान योग प्रत्येक व्यक्ति के लिए सर्वसुलभ और अत्यधिक फलदायी है। इसकी साधना से हर व्यक्ति भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार का सफल जीवन बिता सकता है। हम जिस क्षण जन्म लेते हैं, उसी क्षण से विचारों का सिलसिला प्रारम्भ हो जाता है, जो मृत्यु के क्षण तक चलता रहता है।’’
पातंजलि सूत्रों की संक्षिप्त किन्तु सारगर्भित व्याख्या अत्यन्त सुन्दर एवं सर्वग्राही हैं। साधना पथ की बाधाएँ-‘विक्षेप’ सभी साधकों का अनुभव है। बहुत लोग विचलित हो जाते हैं, जो विक्षेपों को सहज रूप से लेकर चले जाने देते हैं, वे साधना मार्ग पर और अग्रसर होते जाते हैं।
परिशिष्ट में ध्यान साधकों के लिए निर्देश अत्यन्त उत्तम है। मैंने इकट्ठा इन सभी मूल बातों का संकलन नहीं देखा। मस्तिष्क में उठने वाले प्रायः सभी प्रश्नों के उत्तर सूची में दिए गए हैं।
पत्रों के माध्यम से स्वामी परमानन्द जी ने शिष्यों के प्रश्नों का बहुत सरलता से बात-बात में, उत्तर दे दिया है। इन पत्रों में साधारण से दिखने वाली बातों पर जैसे बच्चों के नैसर्गिक व्यवहार एवं खिलौनों में जीवन प्रवाह ढूँढ़ना, आकांक्षा एवं महत्वाकांक्षा में भेद, सुख और साधन के खोज की व्यर्थता, प्रेम भाव का सच्चा प्रवाह जैसे पूर्णतया व्यक्तिगत जैसी दिखने वाली बातों पर कितनी सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया है जिससे साधारण मनुष्य के मस्तिष्क में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। पति-पत्नी की श्रेष्ठता तय करने की व्यर्थता, आध्यात्मिक यात्रा में ‘एकला चलो रे’ का महत्त्व, धर्म और विज्ञान में अनावश्यक संघर्ष की खोज आदि पर अत्यन्त रोचक तरीके से विश्लेषण दिया गया है।
इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य एक सामान्य व्यक्ति के वास्तविक विकास के लिए आध्यात्मिक यात्रा का कितना महत्त्व है इसमें किन मूल बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो प्रश्न उमड़-घुमड़ कर मन में आते हैं, उनका क्या उत्तर है। इन सब बातों पर विचार किया गया है। किसी व्यक्ति के विकास के लिए जो उसे वास्तविक गन्तव्य (मंजिल) की ओर ले जाती हो, जहाँ संघर्ष समाप्त हो जाए, इच्छाओं के पूर्ति की कामना ही न रह जाए, पूरी विवेचना, एक स्थान पर सरल भाषा में इन लेखों और पत्रों में की गयी है। स्वामी परमानन्द जी जितने सरल हैं, वैसी ही उनकी सरल शैली है। मुझे पूरी आशा है कि इससे सभी लाभान्वित होंगे।
जीवन को या स्वयं को समझने के लिए हमारे समाज में युगों-युगों से चितंन होता रहा है। बहुत से ऋषि, मुनियों, दार्शनिकों और चिंतकों ने बहुत-सी पुस्तकें लिखी हैं। हमारी आध्यात्मिक विचारधारा और आध्यात्मिक यात्रा ही हमें विश्व में एक विशेष स्थान प्रदान करती है।
स्वामी परमानन्द जी द्वारा लिखी यह पुस्तक कई तरह से भिन्न है। पहले तो यह स्वयं के अनुभवों पर आधारित है। वे अनुभव हिमालय की गुफा में बैठकर या दूर-दराज के इलाकों में कहीं अलग-थलग कुछ चुने हुए प्रशंसक शिष्यों के बीच के अनुभव नहीं हैं बल्कि भीड़ भरी गलियों, मुहल्लों और सुख-दुख से सनी हुई सामान्य लोगों की बातों के बीच से उत्पन्न अनुभव हैं। उन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त ज्ञान, सामान्य लोगों से मिली जानकारी, गुरुओं और महर्षि महेश योगी जैसे विचारकों के सान्निध्य से प्राप्त समझ से उभरे विश्लेषण शक्ति का उपोयग करके, क्लिष्ट विषयों पर सरलता से विवेचना की है।
हमारे समाज में विचारो में बड़ा द्वन्द्व चलता रहता है। राम बड़े हैं कि कृष्ण। राम और रावण का क्या सम्बन्ध है, क्या कबीर, बुद्ध, महावीर की विचारधाराएँ अलग-अलग हैं ? क्या फर्क है इनमें ? रावण को उसके पाण्डित्य के लिए मान दिया जाए या सीता को चुरा कर राम से युद्ध करने के लिए अपमान। पुनर्जन्म होता है कि नहीं, योग तो कई प्रकार के हैं, प्रचारक या गुरु भी कई हैं, किसे मानें किसे न मानें। कर्मयोगी बनूँ, भक्ति करूँ, हठ योग बनूँ या राजयोग को मानूँ। जीवन में लड़ाई ही लड़ाई है, द्वन्द्व ही द्वन्द्व है। हमारे लिए क्या ठीक है, कैसे चयन करें।
स्वामी परमानन्द जी के लेखों और पत्रों के इस संकलन में बड़ी सरलता से इन प्रश्नों के उत्तर दिये गये हैं, इस तरह कि, जो एक साधारण व्यक्ति के समझ मे आयें।
योग का क्या अर्थ है, शरीर क्यों है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, शरीर को आधार मानकर क्या करना है, कहाँ पहुँचना है। इन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर सरल भाषा में दिया गया है।
मैं विशेष रूप से ‘राम महामन्त्र क्यों ? और ‘मैं कृ़ष्ण का भक्त नहीं हूँ’ जैसे रोचक लेखों का उल्लेख करूँगा। इन लेखों में अत्यन्त सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। भारतीय मनीषियों का सम्यक् जीवन का दृष्टिकोण इतनी अच्छी तरह से बताया गया है जो मैंने कहीं नहीं देखा। कहा है : ‘वैदिक ऋषियों में सभी पत्नी और परिवारयुक्त थे। बुद्ध और महावीर भी विवाहित थे, तथा बुद्ध के संन्यास पूर्व एक पुत्र और महावीर के एक पुत्री थी। गृहस्थ जीवन तथा भौतिक सुख-समृद्धि का प्रयास भी वांछनीय है, पर यही अन्त नहीं है। इसके आगे भी बहुत कुछ पाने को है। जिसने सांसारिक वैभव अर्जित ही नहीं किया, उसका वैभव परित्याग या संसार से वैराग्य की बात करना विरक्ति नहीं मात्र सांत्वना है, मन समझावा। अनासक्ति का आधार पूर्ण तृप्ति होना चाहिए, न कि प्राप्त करने की अक्षमता। जब तक सांसारिक वैभव अर्जित नहीं किया जाता, तब तक यह पता नहीं चलेगा, कि वैभव से तृप्ति नहीं मिलती। कामना तो दुष्पूर है। दूसरों से सुनकर वैभव को नकारना निकम्मापन ही होगा और मन में सदैव उसके लिए रस बना रहेगा।’’
इसी तरह ‘‘अब किसी व्यक्ति की एक उँगली, क्या शरीर की भक्त हो सकती है। जो उसी का भाग है, अंश है, उसके समर्पण का क्या अर्थ है। इसीलिए मैं कृष्ण का भक्त नहीं हूँ।’’
‘‘पुनर्जन्म व्यवस्था’ पर अपने एक शिष्य को लिखे पत्र में स्वामी परमानन्द जी ने साफ कर दिया है, ‘‘मनुष्य एक यात्रा का अन्तिम पड़ाव है, जहाँ से दूसरी यात्रा शुरू होती है। अनन्त की, ब्रह्मत्व की यात्रा, मोक्ष की, निर्वाण की यात्रा। यह यात्रा यदि शुरू नहीं हो पाती तो मनुष्य जन्म मरण के एक दुष्चक में घूमता रहता है।’’
संस्कार क्या हैं एक जन्म से दूसरे जन्म में किस तरह से हस्तान्तरित होते हैं और कब विगलित हो जाते हैं बहुत सरल तरीके से बताया है।
‘‘पंचभौतिक शरीर और संस्कार आवेष्टित मन मिलकर एक व्यक्ति का निर्माण करते हैं और जीवन-यात्रा प्रारम्भ हो जाती है। यह समझ लें कि ‘संस्कार’ क्या है ? और इनका क्या महत्त्व है ? मानसिक वाचिक या शारीरिक प्रत्येक कर्म का कुछ कर्मफल होता है औश्र प्रत्येक कर्मफल मन पर एक संस्कार छोड़ जाता है। यह संस्कार स्मृति का ही अति सूक्ष्म रूप है। संस्कार ही भावी इच्छा या कामना का बीज होता है। कामना या इच्छा से विचार उत्पन्न होता है और विचार कर्म में फलित होता है। इस प्रकार संस्कार-इच्छा-विचार-कर्म-कर्फफल-संस्कार का चक्र अबाध गति से चलता रहता है।....साधना द्वारा संस्कार समूह का विगलन और मन का निर्मलन होते-होते एक दिन योग सिद्ध और संसिद्ध होकर अचानक शून्य में वह छलाँग लग जाती है-या कहें वहाँ विस्फोट हो जाता है जब व्यक्ति का व्यक्तित्व विलीन हो जाता है और वह विराट से एकाकार होकर स्वयं ‘ब्रह्म’ हो जाता है।’’
इन रोचक विषयों पर व्याख्या के बाद ध्यान योग और साधना को इतनी सरलता से समझाया गया कि लगता है, जैसे बातचीत हो रही हो। विलक्षण वाक्य है : ‘‘योग साधना का उद्देश्य है, इन संस्कार ग्रन्थियों का विगलन, नए संस्कार ग्रन्थियों के निर्माण को रोकना और जीवन त्रिभुज को संस्कारों से अलग कर मूल स्थिति में ले आना।’’ फिर राजयोग किस तरह एक गृहस्थ को जीवन के सभी कार्य करने के साथ-साथ आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर करती है, सहज तरीके से बताया गया है। देखिए कितना सरल है : ‘‘मन को विचार से निर्विचार में ले जाने अर्थात विचार को भीतर मोड़कर उसके उद्गगम तक ले जाने की क्रिया को ही ध्यान कहते हैं। इसीलिए यह प्रक्रिया ध्यान योग कहलाती है। ध्यान योग में प्रक्रिया को एक बार समझ लेने पर रोज-रोज किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती। सारी प्रगति स्वतः चालित होती है। मन पर खान-पान, रहन-सहन, तथा सोने-जागने के समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आधुनिक जीवन-पद्धति के हर वर्ग के अनुकूल पड़ता है। किसी भी स्थिति में मन विचार करता ही रहता है। अतः ध्यान वर्ग के अनुकूल पड़ता है। किसी भी स्थिति में मन विचार करता ही रहता है। अतः ध्यान योग की साधना के लिए किसी विशिष्ट स्थान या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं। आप बस में, ट्रेन में या शिप या प्लेन में कहीं भी ध्यान कर सकते हैं। आपको केवल आराम से सुखद आसन में बैठना होता है, वह चाहे कुशा-आसन हो या आरामकुर्सी, तख्त हो या वायुयान की सीट हर जगह ध्यान हो सकता है। इसीलिए यह अधिकार के साथ कहा जा सकता है, कि गृहस्थों तथा आधुनिक जीवन-पद्धति में ध्यान योग प्रत्येक व्यक्ति के लिए सर्वसुलभ और अत्यधिक फलदायी है। इसकी साधना से हर व्यक्ति भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार का सफल जीवन बिता सकता है। हम जिस क्षण जन्म लेते हैं, उसी क्षण से विचारों का सिलसिला प्रारम्भ हो जाता है, जो मृत्यु के क्षण तक चलता रहता है।’’
पातंजलि सूत्रों की संक्षिप्त किन्तु सारगर्भित व्याख्या अत्यन्त सुन्दर एवं सर्वग्राही हैं। साधना पथ की बाधाएँ-‘विक्षेप’ सभी साधकों का अनुभव है। बहुत लोग विचलित हो जाते हैं, जो विक्षेपों को सहज रूप से लेकर चले जाने देते हैं, वे साधना मार्ग पर और अग्रसर होते जाते हैं।
परिशिष्ट में ध्यान साधकों के लिए निर्देश अत्यन्त उत्तम है। मैंने इकट्ठा इन सभी मूल बातों का संकलन नहीं देखा। मस्तिष्क में उठने वाले प्रायः सभी प्रश्नों के उत्तर सूची में दिए गए हैं।
पत्रों के माध्यम से स्वामी परमानन्द जी ने शिष्यों के प्रश्नों का बहुत सरलता से बात-बात में, उत्तर दे दिया है। इन पत्रों में साधारण से दिखने वाली बातों पर जैसे बच्चों के नैसर्गिक व्यवहार एवं खिलौनों में जीवन प्रवाह ढूँढ़ना, आकांक्षा एवं महत्वाकांक्षा में भेद, सुख और साधन के खोज की व्यर्थता, प्रेम भाव का सच्चा प्रवाह जैसे पूर्णतया व्यक्तिगत जैसी दिखने वाली बातों पर कितनी सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया है जिससे साधारण मनुष्य के मस्तिष्क में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। पति-पत्नी की श्रेष्ठता तय करने की व्यर्थता, आध्यात्मिक यात्रा में ‘एकला चलो रे’ का महत्त्व, धर्म और विज्ञान में अनावश्यक संघर्ष की खोज आदि पर अत्यन्त रोचक तरीके से विश्लेषण दिया गया है।
इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य एक सामान्य व्यक्ति के वास्तविक विकास के लिए आध्यात्मिक यात्रा का कितना महत्त्व है इसमें किन मूल बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो प्रश्न उमड़-घुमड़ कर मन में आते हैं, उनका क्या उत्तर है। इन सब बातों पर विचार किया गया है। किसी व्यक्ति के विकास के लिए जो उसे वास्तविक गन्तव्य (मंजिल) की ओर ले जाती हो, जहाँ संघर्ष समाप्त हो जाए, इच्छाओं के पूर्ति की कामना ही न रह जाए, पूरी विवेचना, एक स्थान पर सरल भाषा में इन लेखों और पत्रों में की गयी है। स्वामी परमानन्द जी जितने सरल हैं, वैसी ही उनकी सरल शैली है। मुझे पूरी आशा है कि इससे सभी लाभान्वित होंगे।
सतीश चन्द्र श्रीवास्तव
नई दिल्ली
नई दिल्ली
अपनी बात
सैद्धान्तिक रूप से इस बात की पूरी सम्भावना है कि यदि सागर की कोई लहर ऊपर उठने लगे तो इतने ऊपर तक उठ सकती है कि सागर का सारा जल उस एक लहर में खिंच जाए क्योंकि हर लहर का भीतरी तल सागर के जल से सीधे सम्पर्क में रहता है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति इस अनादि अनन्त निस्सीम सृष्टि में व्याप्त चेतना के सागर की एक-एक लहर ही है जो अपने ऊपर प्रतिबिम्बित होनेवाले विशिष्ट संस्कार समूह के कारण विशिष्ट व्यक्तित्व प्राप्त कर लेती है। प्रत्येक लहर या व्यक्तिगत मन सृष्टि के परा क्षेत्र में स्थित निस्सीम सागर के सम्पर्क में रहता है किन्तु बोध करनेवाले चेतन मन और परा के बीच अचेतन मन का कुचालक अवरोध होने के कारण उसे इसका बोध नहीं होता। इस बोध को प्राप्त करते ही वह लहर इतना विराट हो सकती है कि सारी सृष्टि की चेतना ऊर्जा और मेधा उस एक लहर में समा जाए ऐसी दशा में क्या सृष्टि में चेतना का सागर उस लहर में खो जाएगा और परा शून्य हो जाएगी ! –नहीं।
ईशावास्त्र उपनिषद ने बताया है-पूर्णस्य पूर्णमादय, पूर्णमेवा वशिस्यते।
पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने पर जो बचता है वह भी पूर्ण ही होता है। परा का क्षेत्र निरपेक्ष पूर्ण है। इसलिए इसकी सम्पूर्ण चेतना एक लहर में खिंच जाने पर भी चेतना का सागर सम्पूर्ण ही रहेगा। यह पूर्ण निरपेक्ष क्षेत्र की गणित है। असंख्य सीमित टुकड़े जोड़ देने पर भी जो बनेगा वह सीमित ही रहेगा, निस्सीम नहीं हो सकता और निस्सीम के चाहे जितने टुकड़े कर लें हर निकलनेवाला अंश निस्सीम ही होगा। निस्सीम के योग से ही निस्सीम बन सकता है। भारतीय दर्शन और योग शास्त्र का यह गणित बुद्धि की सीमा से परे है। यह केवल समाधि की अनन्त निस्सीम चेतना में ही बोधगम्य है। इससे यह आश्वासन और संकल्प मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति अखिल ब्रह्मांड का रचमित्व प्राप्त कर ‘अहम् ब्रह्मास्मि’ का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता हुआ ब्राह्मी चेतना में जी सकता है। उसे केवल ध्यान योग की सहज साधना का मार्ग निष्ठापूर्वक अपनाना होगा। मार्ग पकड़ लेने पर बस ‘चरैवेति चरैवेति’। चलते रहो, चलते रहो। मंजिल मिल ही जाएगी। यह मार्ग केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं वरन् उसके पूर्व भौतिक सफलता के लिए भी अनिवार्य है। यह पूर्ण निरपेक्ष क्षेत्र की गणित है। भौतिक सफलता और आध्यात्मिक विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है कि वह सौ प्रतिशत भौतिक और सौ प्रतिशत आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण विकसित स्वरूप का उपभोग करे। इस देश में काल के प्रभाव से अनेक सिद्धान्त एकदम उलटे रूप में प्रचलित हो गए। उपनिषदों के सिद्धान्तों के विपरीत प्रचार और आचरण होने लगा। भौतिक समृद्धि और गृहस्थ जीवन को आध्यात्मिक विकास के विपरीत और बाधक मान लिया गया। लोगों के लिए ‘विद्या’ या अध्यात्म की उपासना के लिए ‘अविद्या’ या भौतिक संसार का परित्याग आवश्यक शर्त बना दिया गया। यह कितना भ्रामक है, यह ईशावास्य उपनिषद के मन्त्रों 9 तथा 11 से स्पष्ट है :
ईशावास्त्र उपनिषद ने बताया है-पूर्णस्य पूर्णमादय, पूर्णमेवा वशिस्यते।
पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने पर जो बचता है वह भी पूर्ण ही होता है। परा का क्षेत्र निरपेक्ष पूर्ण है। इसलिए इसकी सम्पूर्ण चेतना एक लहर में खिंच जाने पर भी चेतना का सागर सम्पूर्ण ही रहेगा। यह पूर्ण निरपेक्ष क्षेत्र की गणित है। असंख्य सीमित टुकड़े जोड़ देने पर भी जो बनेगा वह सीमित ही रहेगा, निस्सीम नहीं हो सकता और निस्सीम के चाहे जितने टुकड़े कर लें हर निकलनेवाला अंश निस्सीम ही होगा। निस्सीम के योग से ही निस्सीम बन सकता है। भारतीय दर्शन और योग शास्त्र का यह गणित बुद्धि की सीमा से परे है। यह केवल समाधि की अनन्त निस्सीम चेतना में ही बोधगम्य है। इससे यह आश्वासन और संकल्प मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति अखिल ब्रह्मांड का रचमित्व प्राप्त कर ‘अहम् ब्रह्मास्मि’ का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता हुआ ब्राह्मी चेतना में जी सकता है। उसे केवल ध्यान योग की सहज साधना का मार्ग निष्ठापूर्वक अपनाना होगा। मार्ग पकड़ लेने पर बस ‘चरैवेति चरैवेति’। चलते रहो, चलते रहो। मंजिल मिल ही जाएगी। यह मार्ग केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं वरन् उसके पूर्व भौतिक सफलता के लिए भी अनिवार्य है। यह पूर्ण निरपेक्ष क्षेत्र की गणित है। भौतिक सफलता और आध्यात्मिक विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है कि वह सौ प्रतिशत भौतिक और सौ प्रतिशत आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण विकसित स्वरूप का उपभोग करे। इस देश में काल के प्रभाव से अनेक सिद्धान्त एकदम उलटे रूप में प्रचलित हो गए। उपनिषदों के सिद्धान्तों के विपरीत प्रचार और आचरण होने लगा। भौतिक समृद्धि और गृहस्थ जीवन को आध्यात्मिक विकास के विपरीत और बाधक मान लिया गया। लोगों के लिए ‘विद्या’ या अध्यात्म की उपासना के लिए ‘अविद्या’ या भौतिक संसार का परित्याग आवश्यक शर्त बना दिया गया। यह कितना भ्रामक है, यह ईशावास्य उपनिषद के मन्त्रों 9 तथा 11 से स्पष्ट है :
अन्धः तमः प्रविशन्ति यो अविद्याभु पासते।
ततो भूव इवते तमो यउ विद्ययायां रताः।। (9)
ततो भूव इवते तमो यउ विद्ययायां रताः।। (9)
जो अविद्या अर्थात् भौतिकवाद की उपासना करते हैं वे अन्धकार में जाते हैं और जो केवल विद्या या अध्यात्मवाद में ही रत रहते हैं वे और भी घने अन्धकार में जाते हैं।
विद्यां च अविद्यांच यस्तद्वेदोभयं सहू।
अविद्यया मृत्युर्तीवा विद्रयया अमृत मश्नुते।। (11)
अविद्यया मृत्युर्तीवा विद्रयया अमृत मश्नुते।। (11)
विद्या तथा अविद्या जो इन दोनों को एक साथ जानते हैं वे अविद्या के द्वारा मृत्यु लानेवाले कारणों या प्रवाहों को पार करते हैं और विद्या के द्वारा अमरत्व को चखते हैं।
अर्थात् मृत्यु लानेवाले या शरीर को नष्ट करनेवाले कारणों, जैसे-रोग, चोट, प्राकृतिक आपदा आदि से अविद्या के द्वारा ही पार पाया जाएगा। जैसे हड्डी टूट जाने पर ध्यान या भजन कीर्तन से हड्डी नहीं जुड़ेगी। शरीर रक्षा तो अविद्या के विभिन्न अंगों, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि से ही होगी। लेकिन शरीर के अन्दर जो शाश्वत अमर तत्त्व है ‘आत्मा’ या ‘चेतना’ उसका स्वाद तो केवल ‘विद्या’ या आध्यात्मिक साधना से ही प्राप्त होगा। यह है भारतीय मनीषियों का सम्यक जीवन का दृष्टिकोण। वैदिक ऋषियों में सभी पत्नी और परिवारयुक्त थे। बुद्ध और महावीर भी विवाहित थे तथा बुद्ध के संन्यास पूर्व एक पुत्र और महावीर के एक पुत्री थी। गृहस्थ जीवन तथा भौतिक सुख-समृद्धि का प्रयास भी वांछनीय है पर यही अन्त नहीं है। इसके आगे भी बहुत कुछ पाने को है। जिसने सांसारिक वैभव अर्जित ही नहीं किया उसका वैभव परित्याग या संसार से वैराग्य की बात करना विरक्ति नहीं मात्र सांत्वना है, मन समझावा। अनासक्ति का आधार पूर्ण तृप्ति होना चाहिए न कि प्राप्त करने की अक्षमता। जब तक सांसारिक वैभव अर्जित नहीं किया जाता तब तक यह पता नहीं चलेगा कि वैभव से तृप्ति नहीं मिलती। कामना तो दुष्पूर है। दूसरों से सुनकर वैभव को नकारना निकम्मापन ही होगा और मन में सदैव उसके लिए रस बना रहेगा।
प्रत्येक मनुष्य, स्त्री-पुरुष का कर्तव्य है कि अपने मन की सम्पूर्ण क्षमता, सम्पूर्ण विभव का विकास ध्यान-योग द्वारा करे और तब उसकी अपार क्षमता का उपयोग कर सांसारिक जीवन में सम्पूर्ण सफलता अर्जित करे। उस सफलता से उसे प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि सब कुछ पा लेने पर भी मन खाली का खाली रह गया। न तृप्ति मिली, न सन्तोष और तब स्वतः संसार का अतिक्रमण कर, मन अमरतत्व का स्वाद लेने के मार्ग पर बढ़ जाएगा। संसार में पूर्ण सफलता के लिए मन की सम्पूर्ण क्षमता का विकास अनिवार्य शर्त है। हमें चारों तरफ जो बहुत से सफल धनी-मानी राजनेता, शासक, प्रशासक, व्यवसायी दिखाई देते हैं वे अतृप्त ही रहते हैं। वे एक अन्धी दौड़ में भाग रहे हैं। क्योंकि वे केवल अपनी जन्मजात मन की क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। उनकी क्षमता अन्य से अधिक है इसलिए वे आगे हैं। पर उनकी अपार क्षमता अभी अविकसित है इसलिए वे अतृप्ति की मृगतृष्णा में भटक रहे हैं। भोग से तृप्ति का मापदंड ही है मोह का अतिक्रमण। ध्यान पर प्रस्तुत चार लेखों का उद्देश्य पूरा हो जाएगा यदि कुछ पाठकों में साधना की प्यास जगाए और साधना के राजमार्ग पर यात्रा प्रारम्भ करने में उनका मार्ग दर्शन कर सके। यात्रा प्रारम्भ करने तक ही सारी अटक है। एक बार यात्रा प्रारम्भ हो जाने पर फिर सब स्वतः होता रहता है।
अन्य सभी लेख विभिन्न ध्यान सत्र में अपने शिष्य, मित्रों के साथ विभिन्न विषयों जैसे-पुनर्जन्म, चातुर्वर्ण व्यवस्था आदि पर हुई चर्चाओं का संक्षिप्त रूप है। ‘राम’ तथा ‘मैं’ कृष्ण का भक्त नहीं हूँ-कुछ वर्ष पूर्व रामनवमी पर दिल्ली के रामलीला मैदान में और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर स्व. न्यायमूर्ति गोपीनाथ के मन्दिर में दिए गए प्रवचन के अंश है। कुछ लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के दिए गए उत्तर में कुछ पत्र भी संकलित हैं। पत्रों में बाल नाट्य विधा की ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ बड़ी बहन रेखाजी को ‘खिलौना’ और नाटक पर लिखे पत्र उन्हीं की प्रेरणा से इस संकलन में रखे गए हैं। इन लेखों और पत्रों के प्रकाशन का विचार मेरे अनुज शिष्य श्री सतीशचन्द्र श्रीवास्तव के मस्तिष्क की उपज है। अपने स्वभाव के अनुसार जैसे अपने विचार को पूरी लगन और निष्ठा से कार्यन्वित करते हैं। वे इस विचार को भी मूर्त रूप देने में जुट गए और उसका फल आपके सामने है।
इन लेखों और पत्रों में मैंने अपने वे विचार प्रस्तुत किए हैं जो अपने अध्ययन, मनन और ध्यानगत चेतना में मुझे समझ में आए। हर व्यक्ति का एक अपना सत्य होता है। इन लेखों और पत्रों का उद्देश्य पाठक के मन में एक कौतूहल, एक जिज्ञासा पैदा करना है कि वह इन विषयों पर सोचे, तर्क करे और शान्तचित्त होकर इन पर अपना निर्णय ले। ये सभी विषय जीवन में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इन पर स्पष्ट समझ होना श्रेयस्कर है। अगर आपकी समझ दूसरों की समझ से मेल नहीं खाती तो चिन्ता न करें आपके लिए अपनी ही समझ उचित है। ‘‘स्वधर्म निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह।’’ आपकी समझ आपके स्वभाव का परिणाम है और वही आपका धर्म है।
अपने स्वर्गीय माता श्रीमती चम्पावती तथा पिता श्री रामानन्द गौड़, अग्रज स्वामी सत्यानन्दजी, ध्यानयोग पुनर्जागरण के प्रवर्तक पूज्य महर्षि महेशयोगीजी तथा प्रातः स्मरणीय गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानन्दजी सरस्वती को शत-शत प्रणाम तथा चरण वन्दना। अपनी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती प्रेमकुमारी को धन्यवाद जो सदैव सहायक रहीं। श्री शरद अग्रवाल का आभारी हूँ जिन्होंने इस ग्रन्थ को वर्तमान स्वरूप में व्यवस्थित किया।
राम महामन्त्र क्यों ?
‘राम’ अत्यन्त विलक्षण शब्द है। साधकों के द्वारा बीज मन्त्र के रूप में ‘राम’ का प्रयोग अनादि काल से हो रहा है और न जाने कितने साधक इस मन्त्र के सहारे परमपद प्राप्त कर चुके हैं। आज ‘राम’ कहते ही दशरथ-पुत्र धनुर्धारी राम का चित्र उभरता है परन्तु ‘राम’ शब्द तो पहले से ही था। तभी तो गरु वशिष्ठ ने दशरथ के प्रथम पुत्र को यह सर्वश्रेष्ठ नाम प्रदान किया। धार्मिक परम्परा में ‘राम’ और ‘ओऽम’ समकक्ष है। ‘ओऽम’ प्रतीकात्मक है और ‘राम’ सार्थक। राम शब्द में आखिर ऐसा क्या है ? इस प्रश्न का यही उत्तर हो सकता है कि ‘राम’ में क्या नहीं है ?
थोड़ा विचार करें। ‘राम’ तीन अक्षरों से मिलकर बना है। र+अ+म ‘राम’ के इन तीन घटक अक्षरों को छः प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है।
र+अ+म = राम
र+म+अ =रमा
म+अ+र = मार (कामदेव)
म+र+अ= मरा
अ+म+र = अमर
अ+र+म = अरम
इस प्रकार देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इन तीन अक्षरों में सृष्टि की उत्पत्ति सृजन प्रसार और विलय सब समाया हुआ है, और इतना ही नहीं यह भी प्रकट हो जाता है कि प्रत्यक्षतः विरोधाभासी दिखनेवाले सब एक ही हैं। मायावश ही उनके विरोध का आभास होता है। विस्तार से देखें- जो ‘राम’ अर्थात् पुरुष हैं वही ‘रमा’ अर्थात् स्त्री या प्रकृति है। ‘राम’ पुरुष रूप में सारी सृष्टि का कारण है, आक्रामक बल है। वही ‘रमा’ स्त्री या प्रकृति के रूप में संग्राहक है सृजन की निर्माणकर्ता है। राम पुरुष बल प्रधान है, ‘रमा’ संवेदना प्रधान। ‘राम’ बुद्धि प्रधान है, विश्लेषणात्मक है। रमा भावना प्रधान है, संश्लेषणात्मक है। बुद्धि मार्ग निर्देश करती है, भावना (‘चित्त’) स्थायित्व प्रदान करती है। सृजन के ये दो आधार हैं। लेकिन जब तक ‘राम’ और ‘रमा’ अलग-अलग रहें सृजन असम्भव है। दोनों नदी के दो पाट हैं। इनको संयुक्त करता है म+अ+र = मार या काम। भगवान बुद्ध द्वारा ‘मार विजय’ की बड़ी प्रशस्ति है, ऋषियों द्वारा काम विजय हमेशा एक आदर्श रहा, नारद मोह का पूरा आख्यान अत्यन्त सारगर्भित है किन्तु ‘मार’ है, तभी उसके परे जाकर परमपद या ‘एकत्व’ प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा राम और रमा, मार द्वारा संयुक्त होकर सृष्टि को फैलाते ही जाएँगे। पुरुष और प्रकृति अलग-अलग नहीं हैं और न उनके परस्पर सम्बन्ध की ही कोई स्वतन्त्र सत्ता है। जो ‘राम’ है वही ‘रमा’ है और वही ‘मार’ है।
अब दूसरा युग्म लें। जो ‘अमर’ है वही ‘मरा’ है। अर्थात् तात्विक दृष्टि से देखें तो अमरत्व और मरणधर्मिता, शाश्वता और क्षणभंगुरता अलग-अलग नहीं हैं। जो क्षणभंगुर दिखाई देता है, जो सतत परिवर्तनशील दिखाई देता है, वही अमर है, शाश्वत है। मृत्यु और परिवर्तन तो आभास मात्र है, बुद्धि द्वारा उत्पन्न भ्रम है। मृत्यु होती ही नहीं। मृत्यु से बड़ा कोई झूठ नहीं। फिर भी अज्ञान की अवस्था में मृत्यु से बड़ा कोई ‘सत्य’ नहीं। अज्ञान की दशा में जो ‘मृत्यु’ है वही ज्ञान की स्थिति में अमरत्व है। जब तक मृत्यु वास्तविकता लग रही है तब तो ‘मरा’ ही है वह जीवित ही कहाँ ? जीवन के प्रवाह के ये दो पक्षों के मूल सत्य, मृत्यु और अमरत्व, ‘अमर’ और ‘मरा’ ‘राम में ही निहित हैं। और साथ ही यह यथार्थ भी कि दोनों एक साथ सदैव उपस्थित हैं। प्रत्येक वस्तु का चरम यथार्थ शाश्वत, नित्य, अपरिवर्तनशील, अमर, अनादि और अनन्त है जब कि उसका आभासी स्वरूप या विवर्त क्षणभंगुर, अनित्य सतत परिवर्तनशील, मरणधर्मा और सीमित है।
अब छठा शब्द बनता है अ+र+म = अरम अर्थात् जिसमें रमा न जा सके। विचित्र बात लगती है कि जिसे विद्वान कहते हैं कि सबमें ‘रमा’ है वह ‘अरम’ कैसे हो गया ? विद्वान और ‘सिद्ध’ में यही भेद है। विद्वान ‘उसे’ देखता है और समझने की चेष्टा करता है। सिद्ध उसे अनुभव करता है और, उसके साथ एकाकार हो जाता है। तुलसीदासजी ने कहा है :
अर्थात् मृत्यु लानेवाले या शरीर को नष्ट करनेवाले कारणों, जैसे-रोग, चोट, प्राकृतिक आपदा आदि से अविद्या के द्वारा ही पार पाया जाएगा। जैसे हड्डी टूट जाने पर ध्यान या भजन कीर्तन से हड्डी नहीं जुड़ेगी। शरीर रक्षा तो अविद्या के विभिन्न अंगों, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि से ही होगी। लेकिन शरीर के अन्दर जो शाश्वत अमर तत्त्व है ‘आत्मा’ या ‘चेतना’ उसका स्वाद तो केवल ‘विद्या’ या आध्यात्मिक साधना से ही प्राप्त होगा। यह है भारतीय मनीषियों का सम्यक जीवन का दृष्टिकोण। वैदिक ऋषियों में सभी पत्नी और परिवारयुक्त थे। बुद्ध और महावीर भी विवाहित थे तथा बुद्ध के संन्यास पूर्व एक पुत्र और महावीर के एक पुत्री थी। गृहस्थ जीवन तथा भौतिक सुख-समृद्धि का प्रयास भी वांछनीय है पर यही अन्त नहीं है। इसके आगे भी बहुत कुछ पाने को है। जिसने सांसारिक वैभव अर्जित ही नहीं किया उसका वैभव परित्याग या संसार से वैराग्य की बात करना विरक्ति नहीं मात्र सांत्वना है, मन समझावा। अनासक्ति का आधार पूर्ण तृप्ति होना चाहिए न कि प्राप्त करने की अक्षमता। जब तक सांसारिक वैभव अर्जित नहीं किया जाता तब तक यह पता नहीं चलेगा कि वैभव से तृप्ति नहीं मिलती। कामना तो दुष्पूर है। दूसरों से सुनकर वैभव को नकारना निकम्मापन ही होगा और मन में सदैव उसके लिए रस बना रहेगा।
प्रत्येक मनुष्य, स्त्री-पुरुष का कर्तव्य है कि अपने मन की सम्पूर्ण क्षमता, सम्पूर्ण विभव का विकास ध्यान-योग द्वारा करे और तब उसकी अपार क्षमता का उपयोग कर सांसारिक जीवन में सम्पूर्ण सफलता अर्जित करे। उस सफलता से उसे प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि सब कुछ पा लेने पर भी मन खाली का खाली रह गया। न तृप्ति मिली, न सन्तोष और तब स्वतः संसार का अतिक्रमण कर, मन अमरतत्व का स्वाद लेने के मार्ग पर बढ़ जाएगा। संसार में पूर्ण सफलता के लिए मन की सम्पूर्ण क्षमता का विकास अनिवार्य शर्त है। हमें चारों तरफ जो बहुत से सफल धनी-मानी राजनेता, शासक, प्रशासक, व्यवसायी दिखाई देते हैं वे अतृप्त ही रहते हैं। वे एक अन्धी दौड़ में भाग रहे हैं। क्योंकि वे केवल अपनी जन्मजात मन की क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। उनकी क्षमता अन्य से अधिक है इसलिए वे आगे हैं। पर उनकी अपार क्षमता अभी अविकसित है इसलिए वे अतृप्ति की मृगतृष्णा में भटक रहे हैं। भोग से तृप्ति का मापदंड ही है मोह का अतिक्रमण। ध्यान पर प्रस्तुत चार लेखों का उद्देश्य पूरा हो जाएगा यदि कुछ पाठकों में साधना की प्यास जगाए और साधना के राजमार्ग पर यात्रा प्रारम्भ करने में उनका मार्ग दर्शन कर सके। यात्रा प्रारम्भ करने तक ही सारी अटक है। एक बार यात्रा प्रारम्भ हो जाने पर फिर सब स्वतः होता रहता है।
अन्य सभी लेख विभिन्न ध्यान सत्र में अपने शिष्य, मित्रों के साथ विभिन्न विषयों जैसे-पुनर्जन्म, चातुर्वर्ण व्यवस्था आदि पर हुई चर्चाओं का संक्षिप्त रूप है। ‘राम’ तथा ‘मैं’ कृष्ण का भक्त नहीं हूँ-कुछ वर्ष पूर्व रामनवमी पर दिल्ली के रामलीला मैदान में और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर स्व. न्यायमूर्ति गोपीनाथ के मन्दिर में दिए गए प्रवचन के अंश है। कुछ लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के दिए गए उत्तर में कुछ पत्र भी संकलित हैं। पत्रों में बाल नाट्य विधा की ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ बड़ी बहन रेखाजी को ‘खिलौना’ और नाटक पर लिखे पत्र उन्हीं की प्रेरणा से इस संकलन में रखे गए हैं। इन लेखों और पत्रों के प्रकाशन का विचार मेरे अनुज शिष्य श्री सतीशचन्द्र श्रीवास्तव के मस्तिष्क की उपज है। अपने स्वभाव के अनुसार जैसे अपने विचार को पूरी लगन और निष्ठा से कार्यन्वित करते हैं। वे इस विचार को भी मूर्त रूप देने में जुट गए और उसका फल आपके सामने है।
इन लेखों और पत्रों में मैंने अपने वे विचार प्रस्तुत किए हैं जो अपने अध्ययन, मनन और ध्यानगत चेतना में मुझे समझ में आए। हर व्यक्ति का एक अपना सत्य होता है। इन लेखों और पत्रों का उद्देश्य पाठक के मन में एक कौतूहल, एक जिज्ञासा पैदा करना है कि वह इन विषयों पर सोचे, तर्क करे और शान्तचित्त होकर इन पर अपना निर्णय ले। ये सभी विषय जीवन में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इन पर स्पष्ट समझ होना श्रेयस्कर है। अगर आपकी समझ दूसरों की समझ से मेल नहीं खाती तो चिन्ता न करें आपके लिए अपनी ही समझ उचित है। ‘‘स्वधर्म निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह।’’ आपकी समझ आपके स्वभाव का परिणाम है और वही आपका धर्म है।
अपने स्वर्गीय माता श्रीमती चम्पावती तथा पिता श्री रामानन्द गौड़, अग्रज स्वामी सत्यानन्दजी, ध्यानयोग पुनर्जागरण के प्रवर्तक पूज्य महर्षि महेशयोगीजी तथा प्रातः स्मरणीय गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानन्दजी सरस्वती को शत-शत प्रणाम तथा चरण वन्दना। अपनी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती प्रेमकुमारी को धन्यवाद जो सदैव सहायक रहीं। श्री शरद अग्रवाल का आभारी हूँ जिन्होंने इस ग्रन्थ को वर्तमान स्वरूप में व्यवस्थित किया।
राम महामन्त्र क्यों ?
‘राम’ अत्यन्त विलक्षण शब्द है। साधकों के द्वारा बीज मन्त्र के रूप में ‘राम’ का प्रयोग अनादि काल से हो रहा है और न जाने कितने साधक इस मन्त्र के सहारे परमपद प्राप्त कर चुके हैं। आज ‘राम’ कहते ही दशरथ-पुत्र धनुर्धारी राम का चित्र उभरता है परन्तु ‘राम’ शब्द तो पहले से ही था। तभी तो गरु वशिष्ठ ने दशरथ के प्रथम पुत्र को यह सर्वश्रेष्ठ नाम प्रदान किया। धार्मिक परम्परा में ‘राम’ और ‘ओऽम’ समकक्ष है। ‘ओऽम’ प्रतीकात्मक है और ‘राम’ सार्थक। राम शब्द में आखिर ऐसा क्या है ? इस प्रश्न का यही उत्तर हो सकता है कि ‘राम’ में क्या नहीं है ?
थोड़ा विचार करें। ‘राम’ तीन अक्षरों से मिलकर बना है। र+अ+म ‘राम’ के इन तीन घटक अक्षरों को छः प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है।
र+अ+म = राम
र+म+अ =रमा
म+अ+र = मार (कामदेव)
म+र+अ= मरा
अ+म+र = अमर
अ+र+म = अरम
इस प्रकार देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इन तीन अक्षरों में सृष्टि की उत्पत्ति सृजन प्रसार और विलय सब समाया हुआ है, और इतना ही नहीं यह भी प्रकट हो जाता है कि प्रत्यक्षतः विरोधाभासी दिखनेवाले सब एक ही हैं। मायावश ही उनके विरोध का आभास होता है। विस्तार से देखें- जो ‘राम’ अर्थात् पुरुष हैं वही ‘रमा’ अर्थात् स्त्री या प्रकृति है। ‘राम’ पुरुष रूप में सारी सृष्टि का कारण है, आक्रामक बल है। वही ‘रमा’ स्त्री या प्रकृति के रूप में संग्राहक है सृजन की निर्माणकर्ता है। राम पुरुष बल प्रधान है, ‘रमा’ संवेदना प्रधान। ‘राम’ बुद्धि प्रधान है, विश्लेषणात्मक है। रमा भावना प्रधान है, संश्लेषणात्मक है। बुद्धि मार्ग निर्देश करती है, भावना (‘चित्त’) स्थायित्व प्रदान करती है। सृजन के ये दो आधार हैं। लेकिन जब तक ‘राम’ और ‘रमा’ अलग-अलग रहें सृजन असम्भव है। दोनों नदी के दो पाट हैं। इनको संयुक्त करता है म+अ+र = मार या काम। भगवान बुद्ध द्वारा ‘मार विजय’ की बड़ी प्रशस्ति है, ऋषियों द्वारा काम विजय हमेशा एक आदर्श रहा, नारद मोह का पूरा आख्यान अत्यन्त सारगर्भित है किन्तु ‘मार’ है, तभी उसके परे जाकर परमपद या ‘एकत्व’ प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा राम और रमा, मार द्वारा संयुक्त होकर सृष्टि को फैलाते ही जाएँगे। पुरुष और प्रकृति अलग-अलग नहीं हैं और न उनके परस्पर सम्बन्ध की ही कोई स्वतन्त्र सत्ता है। जो ‘राम’ है वही ‘रमा’ है और वही ‘मार’ है।
अब दूसरा युग्म लें। जो ‘अमर’ है वही ‘मरा’ है। अर्थात् तात्विक दृष्टि से देखें तो अमरत्व और मरणधर्मिता, शाश्वता और क्षणभंगुरता अलग-अलग नहीं हैं। जो क्षणभंगुर दिखाई देता है, जो सतत परिवर्तनशील दिखाई देता है, वही अमर है, शाश्वत है। मृत्यु और परिवर्तन तो आभास मात्र है, बुद्धि द्वारा उत्पन्न भ्रम है। मृत्यु होती ही नहीं। मृत्यु से बड़ा कोई झूठ नहीं। फिर भी अज्ञान की अवस्था में मृत्यु से बड़ा कोई ‘सत्य’ नहीं। अज्ञान की दशा में जो ‘मृत्यु’ है वही ज्ञान की स्थिति में अमरत्व है। जब तक मृत्यु वास्तविकता लग रही है तब तो ‘मरा’ ही है वह जीवित ही कहाँ ? जीवन के प्रवाह के ये दो पक्षों के मूल सत्य, मृत्यु और अमरत्व, ‘अमर’ और ‘मरा’ ‘राम में ही निहित हैं। और साथ ही यह यथार्थ भी कि दोनों एक साथ सदैव उपस्थित हैं। प्रत्येक वस्तु का चरम यथार्थ शाश्वत, नित्य, अपरिवर्तनशील, अमर, अनादि और अनन्त है जब कि उसका आभासी स्वरूप या विवर्त क्षणभंगुर, अनित्य सतत परिवर्तनशील, मरणधर्मा और सीमित है।
अब छठा शब्द बनता है अ+र+म = अरम अर्थात् जिसमें रमा न जा सके। विचित्र बात लगती है कि जिसे विद्वान कहते हैं कि सबमें ‘रमा’ है वह ‘अरम’ कैसे हो गया ? विद्वान और ‘सिद्ध’ में यही भेद है। विद्वान ‘उसे’ देखता है और समझने की चेष्टा करता है। सिद्ध उसे अनुभव करता है और, उसके साथ एकाकार हो जाता है। तुलसीदासजी ने कहा है :
जानत तुमहिं, तुमहिं होय जाई
बूँद सागर में गिरी तो स्वयं सागर हो गई। जब बूँद बची ही नहीं तो रमेगा कौन ? वह परासत्ता, वह चरम वास्तविकता, वह परब्रह्म तो ‘अरभ’ ही हो सकता है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कुछ भी जानने योग्य है, जो कुछ भी मनन योग्य है, वह सब ‘राम’ शब्द में अन्तर्निहित है। योगियों और सिद्धों ने संकेत दिया है कि ‘ज्ञान’ बाहर से नहीं लिया या दिया जा सकता। यह तो अन्दर से प्रस्फुटित होता है। अत्मा सर्वज्ञ है। साधना के प्रभाव से किसी भी शब्द में निहित सारे अर्थ स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ‘सोई जाने जेहि देहु जनाई’ (तुलसीदासजी) इस विराट अर्थवत्ता के कारण ही ‘राम’ महामन्त्र और उसके अनवरत जप से कालान्तर में निहित सार, अर्थ और सृष्टि के सारे रहस्य स्वतः प्रकट होकर साधक को जीवन मुक्त का परमपद प्रदान करते हैं।
इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कुछ भी जानने योग्य है, जो कुछ भी मनन योग्य है, वह सब ‘राम’ शब्द में अन्तर्निहित है। योगियों और सिद्धों ने संकेत दिया है कि ‘ज्ञान’ बाहर से नहीं लिया या दिया जा सकता। यह तो अन्दर से प्रस्फुटित होता है। अत्मा सर्वज्ञ है। साधना के प्रभाव से किसी भी शब्द में निहित सारे अर्थ स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ‘सोई जाने जेहि देहु जनाई’ (तुलसीदासजी) इस विराट अर्थवत्ता के कारण ही ‘राम’ महामन्त्र और उसके अनवरत जप से कालान्तर में निहित सार, अर्थ और सृष्टि के सारे रहस्य स्वतः प्रकट होकर साधक को जीवन मुक्त का परमपद प्रदान करते हैं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book