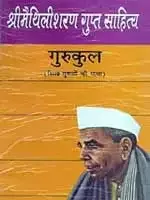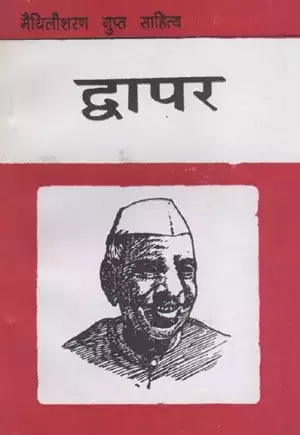|
कविता संग्रह >> गुरुकुल गुरुकुलमैथिलीशरण गुप्त
|
386 पाठक हैं |
||||||
इसमें सिख गुरुओं की गाथा का अलौकिक वर्णन किया गया है।...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
उपोद्घात
लिखने की धुन कहिए अथवा महापुरुषों की ओर हृदय का आकर्षण कहिए, लेखक को
अपने साहित्यिक जीवन के आरम्भ में न जाने, किन-किन विषयों पर लिखने की
उमंग उठा करती थी। महच्चरित्र संसार के किसी भी भू-भाग पर उद्भूत हों, वे
सार्वभौमिक होते हैं। इसलिए महाराणा प्रताप सिंह, छत्रपति शिवाजी और गुरु
गोविन्दसिंह तक ही लेखक की वह लालसा सीमित न थी। हजरत हसन हुसेन पर भी
अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिए उसका हृदय उत्कण्ठित हुआ करता था। उन
दिनों की आरम्भ की हुई कुछ रचनाएँ अब तक पूरी नहीं हुईं। कौन जाने, कभी
होंगी या नहीं। बहुत दिनों तक दुर्बल मस्तक से अतिरिक्त काम लेने के कारण
स्वास्थ्य ऐसा भंग हो गया है कि वे मनोरथ प्रातःकालीन स्वप्नों के समान
अथवा दरिद्रों के मनोरथों की भाँति धीरे-धीरे विलीन हो रहे हैं। इधर
हिन्दी की कवि-प्रवृत्ति भी एक नये मार्ग पर ऐसे वेग से बढ़ रही है कि
लेखक आप ही आप पिछड़ रहा है। उसे इसकी चिन्ता नहीं। चिन्ता इसी बात की है
कि अधूरी रचनाओं के रूप में उसकी कुछ इच्छाएँ पूरी हो जायँ तो उनके लिए
पुनर्जन्म न लेना पड़े और, इस प्रकार, अनाधिकार चेष्टा से उसे इसी जन्म
में ‘मुक्ति’ मिल जाय !
तथापि, इधर, इस पुस्तक के लिखने की कोई सम्भावना न थी। किन्तु थोड़े दिन हुए एक सिख सज्जन ने बड़े स्नेह, आदर और साथ ही कुछ अभिमान पूर्वक लेखक से कहा था-‘‘क्या आप सिख गुरुओं पर भी कुछ लिखने की कृपा करेंगे ? हिन्दी के कवियों ने, कहना चाहिए कि अब तक उन पर कुछ नहीं लिखा। क्या गुरुओं के बलिदान इस योग्य नहीं कि मैं आपसे यह प्रार्थना न कर सकूँ?’’ राम ! राम ! सिख गुरुओं के बलिदान तो ऐसे हैं कि जैसे कुछ होने चाहिए। लेखक बड़े असमंजस में पड़ गया। अपनी असमर्थता अथवा अयोग्यता की बात कहने का भी उसे साहस न हुआ। विवश होकर उसने यही निश्चय किया कि जब तक कोई काव्य-रचना न हो तब तक यह पद्म-रचना ही सही। लेखक का अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धांज्जलि देने का अधिकार तो सर्वथा अक्षुण्य है। अस्तु।
लिखने का निश्चय होने के साथ ही पुस्तक के नामकरण की बात आई। सहसा ‘‘रघुवंश’’ की ओर लेखक का ध्यान गया। सोचा कि उसी के अनुकरण पर ‘गुरुवंश’’ नाम देकर लिखना आरम्भ कर दिया जाय। परन्तु केवल नाम रखने ही से ही क्या होगा ? वैसी कथावस्तु और वैसी वर्णना भी तो होनी चाहिए। छोटे-छोटे अनुष्टुप छन्दों में भी जो चमत्कार वहाँ दिखाई देता है उसका आभास भी यहाँ कहाँ से आवेगा ? फिर ‘नाम बड़े, दर्शन थोड़े’ की कहावत चरितार्थ करने से क्या लाभ ? तब सोचा, न हो ‘गुरुशिष्य’ नाम दिया जाय। परन्तु ‘सिक्ख’ यद्यपि शिष्य से ही बना कहा जाता है परन्तु वह उससे सर्वदा स्वतन्त्र-सा दिखाई देता है। मानो यह नाम भी इतना सपूत निकला कि अपने पिता के नाम से परिचित होने की इसके लिए अपेक्षा नहीं। स्वयं मूल नाम ही इसकी सम्बन्ध-कामना करता है। अन्त में अपने एक आध मित्र के विरोध करने पर भी पुस्तक का नाम ‘‘गुरुकुल’’ रखने का निश्चय किया गया। गुरुकुल एक संस्था विशेष का बोधक होने पर भी उपयुक्त जान पड़ा। क्योंकि सिक्खों के सम्बन्धों में वह गुरुकुल भी तो वैसी ही संस्था है।
तथापि, इधर, इस पुस्तक के लिखने की कोई सम्भावना न थी। किन्तु थोड़े दिन हुए एक सिख सज्जन ने बड़े स्नेह, आदर और साथ ही कुछ अभिमान पूर्वक लेखक से कहा था-‘‘क्या आप सिख गुरुओं पर भी कुछ लिखने की कृपा करेंगे ? हिन्दी के कवियों ने, कहना चाहिए कि अब तक उन पर कुछ नहीं लिखा। क्या गुरुओं के बलिदान इस योग्य नहीं कि मैं आपसे यह प्रार्थना न कर सकूँ?’’ राम ! राम ! सिख गुरुओं के बलिदान तो ऐसे हैं कि जैसे कुछ होने चाहिए। लेखक बड़े असमंजस में पड़ गया। अपनी असमर्थता अथवा अयोग्यता की बात कहने का भी उसे साहस न हुआ। विवश होकर उसने यही निश्चय किया कि जब तक कोई काव्य-रचना न हो तब तक यह पद्म-रचना ही सही। लेखक का अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धांज्जलि देने का अधिकार तो सर्वथा अक्षुण्य है। अस्तु।
लिखने का निश्चय होने के साथ ही पुस्तक के नामकरण की बात आई। सहसा ‘‘रघुवंश’’ की ओर लेखक का ध्यान गया। सोचा कि उसी के अनुकरण पर ‘गुरुवंश’’ नाम देकर लिखना आरम्भ कर दिया जाय। परन्तु केवल नाम रखने ही से ही क्या होगा ? वैसी कथावस्तु और वैसी वर्णना भी तो होनी चाहिए। छोटे-छोटे अनुष्टुप छन्दों में भी जो चमत्कार वहाँ दिखाई देता है उसका आभास भी यहाँ कहाँ से आवेगा ? फिर ‘नाम बड़े, दर्शन थोड़े’ की कहावत चरितार्थ करने से क्या लाभ ? तब सोचा, न हो ‘गुरुशिष्य’ नाम दिया जाय। परन्तु ‘सिक्ख’ यद्यपि शिष्य से ही बना कहा जाता है परन्तु वह उससे सर्वदा स्वतन्त्र-सा दिखाई देता है। मानो यह नाम भी इतना सपूत निकला कि अपने पिता के नाम से परिचित होने की इसके लिए अपेक्षा नहीं। स्वयं मूल नाम ही इसकी सम्बन्ध-कामना करता है। अन्त में अपने एक आध मित्र के विरोध करने पर भी पुस्तक का नाम ‘‘गुरुकुल’’ रखने का निश्चय किया गया। गुरुकुल एक संस्था विशेष का बोधक होने पर भी उपयुक्त जान पड़ा। क्योंकि सिक्खों के सम्बन्धों में वह गुरुकुल भी तो वैसी ही संस्था है।
सिक्ख इसी गुरुकुल में पढ़कर
प्राप्त कर सके हैं वह सत्व,
जीवन-रण-क्षेत्र में बढ़कर
जिससे उन्हें मिला अमरत्व।
प्राप्त कर सके हैं वह सत्व,
जीवन-रण-क्षेत्र में बढ़कर
जिससे उन्हें मिला अमरत्व।
आर्य-समाज के सम्बन्ध के कारण गुरुकुल नाम
एक देशीय हो उठा है। अतएव धार्मिक विवाद के कारण यह भिन्न सम्प्रदाय वालों
के निकट अप्रिय न होने पावे, इस कारण से भी लेखक ने इसे रखना उचित समझा।
लेखक और कुछ नहीं कर सकता था तो वीरों का यशोगान करने के लिए वीर वृत्त चुनना तो उसके वश की बात थी। परन्तु उसने चतुष्पद वृत्त को द्विपद रूप में ग्रहण किया है। कहा नहीं जा सकता है कि यह उसका हास है या विकास ! परन्तु आरम्भ में ही पाठक देखेंगे कि मंगलाचरण की बात दो पंक्तियों में कहने की थी तो उसे खींच-तान कर चार पंक्तियों में ले जाने की आवश्यकता न थी। कथा किंवा वर्णना मूलक प्रबन्धों में यही क्रम लेखक को ठीक जान पड़ता है। फिर भी प्रत्येक पद्य दो पंक्तियों में न छाप कर चार पंक्तियों में छापा गया है।
धारावाहिक वर्णन में जैसा एक पद्य का क्रम आगे के पद्यों में चला जाता है वैसा ही यहाँ भी हुआ। ऐसे स्थलों पर जैसे संस्कृत में युग्म, कलापक और कुलक छन्द समझ लिये जाते हैं वैसे ही हिन्दी में भी माने जा सकते हैं।
छन्द के अनन्तर भाषा के सम्बन्ध में लेखक की क्षुद्र सम्मति है कि इतने दिनों में, बोल-चाल की भाषा ने कविता की भाषा बनने का अपना जन्म-जात अधिकार सिद्ध कर दिखाया है। यह भी कहा जा सकता है कि उसने इस विषय में ‘स्वराज्य’ प्राप्त कर लिया। जहाँ पहले खड़ी बोली में कविता करने का घोर विरोध किया जाता था वहाँ अब यही सुनाई पड़ता है कि ‘‘खड़ी बोली में अवश्य कविता की जाय, परन्तु ब्रजभाषा को न भुलाया जाय’’ निस्सन्देह वह भुलाने योग्य नहीं। वह हिन्दी कवियों की वैदिक भाषा है ! ऋचाओं की भाँति हमारे लिए पवित्र है। यों तो वैदिक भाषा बोलने वाले भी सब मन्त्रकार ही थोड़े ही रहे होंगे। तथापि हमें अपने पूर्वजों की थाती को नष्ट न होने देना चाहिए। सच पूछिए तो वही तो हमारी सम्पत्ति है, जिसे सैकड़ों वर्ष के परिश्रम से हमारे पुरखों ने उपार्जित करके हमें दिया है।
मान लिया कि बोल-चाल की भाषा ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त कर लिया। पर अब संघर्ष छोड़कर उसे स्वराज्य की व्यवस्था भी तो करनी चाहिए। जिस बड़े पद को उसने प्राप्त किया है उसका निर्वाह भी तो उसे करना चाहिए। विजय के अनन्तर शान्ति की स्थापना भी आवश्यक है। किसी भी भाषा की योग्यता उसकी शब्द-सम्पत्ति पर अवलम्बित है। विपुल अर्थ के लिए विपुल शब्द-भण्डार होना चाहिए। सुश्राव्य होना भी भाषा का एक बड़ा गुण है, किन्तु यह भी उसके शब्दों पर अवलम्बित रहता है। उपयुक्त अर्थ के लिए उपयुक्त शब्द होने से श्रुति-सुखदता आप ही आप उत्पन्न हो जाती है।
बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिन्दी में भिन्न-भिन्न प्रकार के कोषों की रचना हो रही है। बोल-चाल की भाषा की कविता का शब्द भण्डार भरने में अपनी प्रान्तिक भाषाओं से भी सहायता लेकर हमें उनसे सम्बन्ध-सूत्र बनाये रखना उचित जान पड़ता है। बृज, बुन्देलखण्डी और अवधी की तो बात ही जाने दीजिए; उन्हें तो हम लोग अपने घरों और गाँवों में नित्य बोलते ही हैं, लेखक की राय में तो अन्य प्रान्तिक भाषाओं में से हमें शब्द ‘जोगाड़’ करते हुए ‘सिहरने’ के बदले ‘विभोर’ ही होना चाहिए! परन्तु यह काम लेखक जैसे लोगों का नहीं; जिनके कान पक्के हों वही शब्द-झंकार को पहचान सकते हैं।
शब्द बोलते हुए संकेत हैं। जिस भाषा में भिन्न-भिन्न भावों और क्रियाओं के लिए भिन्न-भिन्न शब्द न हों वह कभी पूर्ण भाषा नहीं हो सकती।
हमारी प्रान्तिक बोलियों में कभी-कभी ऐसे अर्थपूर्ण शब्द मिल जाते हैं जिनके पर्याय हिन्दी में नहीं मिलते। जब हम अरबी, फारसी और अँगरेजी के शब्द निस्संकोच भाव से स्वीकार करते हैं तब आवश्यक होने पर अपनी प्रान्तीय भाषाओं से उपयुक्त शब्द ग्रहण करने में हमें क्यों संकोच होना चाहिए।
गुरुकुल में एक पंक्ति इस प्रकार है-
लेखक और कुछ नहीं कर सकता था तो वीरों का यशोगान करने के लिए वीर वृत्त चुनना तो उसके वश की बात थी। परन्तु उसने चतुष्पद वृत्त को द्विपद रूप में ग्रहण किया है। कहा नहीं जा सकता है कि यह उसका हास है या विकास ! परन्तु आरम्भ में ही पाठक देखेंगे कि मंगलाचरण की बात दो पंक्तियों में कहने की थी तो उसे खींच-तान कर चार पंक्तियों में ले जाने की आवश्यकता न थी। कथा किंवा वर्णना मूलक प्रबन्धों में यही क्रम लेखक को ठीक जान पड़ता है। फिर भी प्रत्येक पद्य दो पंक्तियों में न छाप कर चार पंक्तियों में छापा गया है।
धारावाहिक वर्णन में जैसा एक पद्य का क्रम आगे के पद्यों में चला जाता है वैसा ही यहाँ भी हुआ। ऐसे स्थलों पर जैसे संस्कृत में युग्म, कलापक और कुलक छन्द समझ लिये जाते हैं वैसे ही हिन्दी में भी माने जा सकते हैं।
छन्द के अनन्तर भाषा के सम्बन्ध में लेखक की क्षुद्र सम्मति है कि इतने दिनों में, बोल-चाल की भाषा ने कविता की भाषा बनने का अपना जन्म-जात अधिकार सिद्ध कर दिखाया है। यह भी कहा जा सकता है कि उसने इस विषय में ‘स्वराज्य’ प्राप्त कर लिया। जहाँ पहले खड़ी बोली में कविता करने का घोर विरोध किया जाता था वहाँ अब यही सुनाई पड़ता है कि ‘‘खड़ी बोली में अवश्य कविता की जाय, परन्तु ब्रजभाषा को न भुलाया जाय’’ निस्सन्देह वह भुलाने योग्य नहीं। वह हिन्दी कवियों की वैदिक भाषा है ! ऋचाओं की भाँति हमारे लिए पवित्र है। यों तो वैदिक भाषा बोलने वाले भी सब मन्त्रकार ही थोड़े ही रहे होंगे। तथापि हमें अपने पूर्वजों की थाती को नष्ट न होने देना चाहिए। सच पूछिए तो वही तो हमारी सम्पत्ति है, जिसे सैकड़ों वर्ष के परिश्रम से हमारे पुरखों ने उपार्जित करके हमें दिया है।
मान लिया कि बोल-चाल की भाषा ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त कर लिया। पर अब संघर्ष छोड़कर उसे स्वराज्य की व्यवस्था भी तो करनी चाहिए। जिस बड़े पद को उसने प्राप्त किया है उसका निर्वाह भी तो उसे करना चाहिए। विजय के अनन्तर शान्ति की स्थापना भी आवश्यक है। किसी भी भाषा की योग्यता उसकी शब्द-सम्पत्ति पर अवलम्बित है। विपुल अर्थ के लिए विपुल शब्द-भण्डार होना चाहिए। सुश्राव्य होना भी भाषा का एक बड़ा गुण है, किन्तु यह भी उसके शब्दों पर अवलम्बित रहता है। उपयुक्त अर्थ के लिए उपयुक्त शब्द होने से श्रुति-सुखदता आप ही आप उत्पन्न हो जाती है।
बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिन्दी में भिन्न-भिन्न प्रकार के कोषों की रचना हो रही है। बोल-चाल की भाषा की कविता का शब्द भण्डार भरने में अपनी प्रान्तिक भाषाओं से भी सहायता लेकर हमें उनसे सम्बन्ध-सूत्र बनाये रखना उचित जान पड़ता है। बृज, बुन्देलखण्डी और अवधी की तो बात ही जाने दीजिए; उन्हें तो हम लोग अपने घरों और गाँवों में नित्य बोलते ही हैं, लेखक की राय में तो अन्य प्रान्तिक भाषाओं में से हमें शब्द ‘जोगाड़’ करते हुए ‘सिहरने’ के बदले ‘विभोर’ ही होना चाहिए! परन्तु यह काम लेखक जैसे लोगों का नहीं; जिनके कान पक्के हों वही शब्द-झंकार को पहचान सकते हैं।
शब्द बोलते हुए संकेत हैं। जिस भाषा में भिन्न-भिन्न भावों और क्रियाओं के लिए भिन्न-भिन्न शब्द न हों वह कभी पूर्ण भाषा नहीं हो सकती।
हमारी प्रान्तिक बोलियों में कभी-कभी ऐसे अर्थपूर्ण शब्द मिल जाते हैं जिनके पर्याय हिन्दी में नहीं मिलते। जब हम अरबी, फारसी और अँगरेजी के शब्द निस्संकोच भाव से स्वीकार करते हैं तब आवश्यक होने पर अपनी प्रान्तीय भाषाओं से उपयुक्त शब्द ग्रहण करने में हमें क्यों संकोच होना चाहिए।
गुरुकुल में एक पंक्ति इस प्रकार है-
कंकण नहीं, मुझे तो कर दो,
जो वैरी को धरें समेट।
जो वैरी को धरें समेट।
समेट धरना बुन्देलखण्डी मुहावरा है। इसके बदले यह भी लिखा जा सकता था-
कंकड़ नहीं, मुझे तो कर दो,
करें शत्रु का जो आखेट।
करें शत्रु का जो आखेट।
परन्तु समेट धरने में एक विशेष अर्थ है।
इसमें शत्रु को पछाड़ देने के साथ-साथ उसे सब ओर से दबा बैठने का भी चित्र
खिंचता है, इसी कारण लेखक इसे रखने का लोभ-संवरण न कर सका। इसलिए वह
क्षमाप्रार्थी है। क्योंकि यह प्रान्तिक प्रयोग है। तथापि एक प्रार्थना
है-इस सम्बन्ध में हमें अपने ही पैरों खड़े होना चाहिए। जैसे वन्ध्या का
बाँझ रूप तो हमारे लिए शिष्ट प्रयोग है परन्तु उसी प्रकार सन्ध्या का सांझ
वैसा नहीं। उसकी अपेक्षा ‘शाम’ अधिक प्रयुक्त है।
अच्छे से अच्छे शब्द को प्रयोग में न लाइए तो वह कुछ दिनों में शिष्ट न रह
जायगा और साधारण शब्द भी व्यवहार में आने से कुछ दिनों में विशिष्ट बन
जायेगा।
लेखक का यह अभिप्राय नहीं कि ‘शाम’ का बहिष्कार कर दिया जाय। जो शब्द भिन्न भाषाओं के होने पर भी हमारी भाषा में मिल गये हैं वे हमारे ही हो गये हैं। परन्तु यह अवश्य कहा जायेगा कि उनके सामने, उसी अर्थ के, अपने शब्दों को अशिष्ट समझना हमारे मन की नहीं तो कानों की गुलामी जरूर है ! आजकल राजनीति की सभाओं में बहुधा एक बात देखी जाती है। वह हिन्दी शब्दों का चुन-चुन कर बहिष्कार और उनके बदले उर्दू-फारसी के अलफाज का प्रचार। हिन्दी के हितचिन्तकों को सावधान हो जाना चाहिए। अपनी भाषा को छोड़ कर हम अपने भावों की रक्षा नहीं कर सकते।
साधारण बोल-चाल की भाषा से लिखने की भाषा में कुछ न कुछ अन्तर होता ही है। इसी प्रकार गद्य की भाषा की अपेक्षा पद्य की भाषा में कुछ अन्तर रहता है। पद्यकारों को एक अर्थ के अनेक शब्दों के प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें और भी कुछ छूट मिलती है। संस्कृत में आवश्यकता होने पर ड और ल, ब और व एवं श और ष में अभेद मान लिया जाता है। कालिदास जैसे कवि को भी वह छूट लेनी पड़ी-
लेखक का यह अभिप्राय नहीं कि ‘शाम’ का बहिष्कार कर दिया जाय। जो शब्द भिन्न भाषाओं के होने पर भी हमारी भाषा में मिल गये हैं वे हमारे ही हो गये हैं। परन्तु यह अवश्य कहा जायेगा कि उनके सामने, उसी अर्थ के, अपने शब्दों को अशिष्ट समझना हमारे मन की नहीं तो कानों की गुलामी जरूर है ! आजकल राजनीति की सभाओं में बहुधा एक बात देखी जाती है। वह हिन्दी शब्दों का चुन-चुन कर बहिष्कार और उनके बदले उर्दू-फारसी के अलफाज का प्रचार। हिन्दी के हितचिन्तकों को सावधान हो जाना चाहिए। अपनी भाषा को छोड़ कर हम अपने भावों की रक्षा नहीं कर सकते।
साधारण बोल-चाल की भाषा से लिखने की भाषा में कुछ न कुछ अन्तर होता ही है। इसी प्रकार गद्य की भाषा की अपेक्षा पद्य की भाषा में कुछ अन्तर रहता है। पद्यकारों को एक अर्थ के अनेक शब्दों के प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें और भी कुछ छूट मिलती है। संस्कृत में आवश्यकता होने पर ड और ल, ब और व एवं श और ष में अभेद मान लिया जाता है। कालिदास जैसे कवि को भी वह छूट लेनी पड़ी-
भुजलतां जलतामबलाजनः
इसमें जड़ता के स्थान में अनुप्रास की
रक्षा के लिए जलता लिखा गया है। तथापि एक नियम के साथ। इस कारण इस सम्बन्ध
में हमें सावधान रहना होगा।
घबड़ाना और घबराना तथा पिंजड़ा और पिंजरा दोनों का योग हिन्दी में होता है। झड़ना लिखने के बदले झरना भी लिखा जा सकता है परन्तु इसी प्रकार झगड़ा का झगरा नहीं लिखा जा सकता।
हम लोग चाहें तो अधिक सम्मति से कुछ नियम बना सकते हैं। जैसे ड और ल के अभेद को छोड़ ऊपर का संस्कृत-नियम हिन्दी में भी मान्य हो सकता है ण और न का अभेद भी माना जा सकता है। विशेष कर पद्य में। इस प्रकार उर्दू-फारसी के शब्दों के प्रयोग में यदि क़ ख़ ग़ और ज़ आदि के नीचे की बिन्दी निकाल दी जाय तो वे मानो संस्कृत होकर हिन्दी के ही बन जायँ। पद्य में उनका प्रयोग बहुत अच्छा मालूम होता है। पर जवादानी में तो अन्तर पड़ने की आशंका नहीं ? बँगला भाषा भिन्न भाषा के शब्दों को अपनाना खूब जानती है।
परन्तु ये सब बातें विद्वानों के विचार करने की हैं। लेखक इस ओर उनका ध्यान मात्र आकर्षित करके अपने दो एक प्रान्तिक प्रयोगों के लिए क्षमा-प्रार्थी है।
घबड़ाना और घबराना तथा पिंजड़ा और पिंजरा दोनों का योग हिन्दी में होता है। झड़ना लिखने के बदले झरना भी लिखा जा सकता है परन्तु इसी प्रकार झगड़ा का झगरा नहीं लिखा जा सकता।
हम लोग चाहें तो अधिक सम्मति से कुछ नियम बना सकते हैं। जैसे ड और ल के अभेद को छोड़ ऊपर का संस्कृत-नियम हिन्दी में भी मान्य हो सकता है ण और न का अभेद भी माना जा सकता है। विशेष कर पद्य में। इस प्रकार उर्दू-फारसी के शब्दों के प्रयोग में यदि क़ ख़ ग़ और ज़ आदि के नीचे की बिन्दी निकाल दी जाय तो वे मानो संस्कृत होकर हिन्दी के ही बन जायँ। पद्य में उनका प्रयोग बहुत अच्छा मालूम होता है। पर जवादानी में तो अन्तर पड़ने की आशंका नहीं ? बँगला भाषा भिन्न भाषा के शब्दों को अपनाना खूब जानती है।
परन्तु ये सब बातें विद्वानों के विचार करने की हैं। लेखक इस ओर उनका ध्यान मात्र आकर्षित करके अपने दो एक प्रान्तिक प्रयोगों के लिए क्षमा-प्रार्थी है।
चली न उनकी एक चाल भी
बिगड़ गई उनकी सब औज।
बिगड़ गई उनकी सब औज।
इसमें
‘‘औज’’ के बदले
‘‘मौज’’ शब्द रक्खा जा सकता था,
परन्तु ‘‘औज’’ में हौसला और
सूझ-बूझ दोनों का भाव भरा हुआ है। इसमें शत्रुओं के किंकर्तव्यविमूढ़ होने
का अर्थ नहीं किन्तु उसके फलस्वरूप उनके चेहरों पर हवाई जड़ने का भी चित्र
अंकित है।
तोड़ मरोड़ उखाड़ पछाड़े
बड़े बड़े बहु अज्झड़ झाड़।
बड़े बड़े बहु अज्झड़ झाड़।
अज्झड़ शब्द में विशाल, भारी और सघन तीनों
अर्थों का समावेश है। इसलिए वह झाड़ों की विशेषण के लिए लेखक को बहुत ही
उपयुक्त मालूम पड़ा।
ऊपर समेट धरने के सम्बन्ध में लिखा जा चुका है। एक दूसरी पंक्ति और सुनिए-
ऊपर समेट धरने के सम्बन्ध में लिखा जा चुका है। एक दूसरी पंक्ति और सुनिए-
‘‘रपट पड़े की हर गंगा’’ में
मिट सकता है क्या उपहास !
मिट सकता है क्या उपहास !
‘‘रपट पड़े की हर
गंगा’’ एक कहावत है, जो इस ओर प्रसंगानुसार कही जाती
है। मालूम नहीं, और कहीं इसका प्रचार है या नहीं। किसी ढंग से अपनी कमजोरी
छिपाने के सम्बन्ध में इसका प्रयोग होता है। एक जन फिसल कर अचानक पानी में
गिर पड़ा। दूसरे देखने वाले कहीं हँसी न करें, यह सोचकर ‘हर
गंगा’-‘हर हर गंगा’ कह कर वह स्नान करने का
अभिनय करने लगा। किन्तु लोग कब चूकने वाले थे ? कह उठे-अजी, यह तो रिपट
पड़े की हर गंगा’ है !
भाषा यथा सम्भव सरल रखने की चेष्टा की गई है। परन्तु इस सम्बन्ध में पाठकों से एक निवेदन करना है। पुस्तक में एक पंक्ति पहले इस प्रकार थी-
भाषा यथा सम्भव सरल रखने की चेष्टा की गई है। परन्तु इस सम्बन्ध में पाठकों से एक निवेदन करना है। पुस्तक में एक पंक्ति पहले इस प्रकार थी-
किन्तु साँप सीधा होकर भी
नहीं छोड़ता है गति वक्र।
नहीं छोड़ता है गति वक्र।
बाद में यह इस प्रकार बदल दी गई-
पर द्विजिह्व सीधा होकर भी
नहीं छोड़ता है गति वक्र।
नहीं छोड़ता है गति वक्र।
द्विजिह्व शब्द जहाँ अधिक उपयुक्त जान
पड़ा। वे मुसलमान जो बन्दा की अधीनता में रहते थे भीतर ही भीतर नवाब से
मिले हुए थे। अतएव उनके लिए द्विजिह्व पद अधिक अर्थसूचक जान पड़ा। चुगलखोर
के अर्थ में भी वह आता है।
फैली कृषि युत कृषिग्रासिनी
घास-राशि-सी पश्वाशक्ति।
यहाँ ‘कृषिग्रासिनी’
के स्थान में ‘कृषिविनाशिनी’ भी कहा जा सकता था,
परन्तु लेखक को इसमें वह ओज नहीं दिखाई दिया।
एक पंक्ति इस प्रकार है-
एक पंक्ति इस प्रकार है-
बलगौरव के करलाघव के
सूक्ष्मदृष्टि के हुए प्रमाण।
सूक्ष्मदृष्टि के हुए प्रमाण।
इसमें क्रम के अनुसार सूक्ष्मदृष्टि के
बदले दृष्टि-सौक्ष्म्य उचित होता। परन्तु व्यर्थ क्लिष्टता से बचने के लिए
वैसा ही रहने दिया गया।
भाई, किधर जा रहे हो तुम
अपना ओक-लोक सब छोड़।
‘‘ओक-लोक’’ कुछ क्लिष्ट होने पर भी घर-वार से अधिक अर्थ वाले एक नये मुहाविरे के रूप में रक्खा गया है।
गुरुओं के सम्बन्ध में लेखक ने यथा-सम्भव श्रद्धापूर्वक ही लिखने का प्रयत्न किया है। इसलिए पक्षकारों के सम्बन्ध में कच्छ और कृपाण के समान कड़ा, केश और कंघी का महत्त्व स्वयं न मानते हुए भी उनके विषय में युक्तियों की कल्पना की गई है। कंधे का तो स्वतन्त्र कोई अस्तित्व ही नहीं। इसलिए केशों को ही ‘‘कंघी के संगी’’ कह कर सन्तोष कर लिया गया है।
महापुरुषों के विषय में अलौकिक बातों की प्रसिद्धि स्वाभाविक है। परन्तु आश्चर्य तो इस बात का है कि गुरु प्रायः करामातों से बराबर इन्कार करते रहे; तब भी उनके सम्बन्ध में ऐसी बातों की चर्चा नहीं रुकी। महापुरुषों में विशेष शक्ति का होना लेखक को अमान्य नहीं। किन्तु इस सम्बन्ध में उसने गुरु नानक जी और गुरु तेगबहादुर जी के आदेश का पालन किया है। कहते हैं, गुरु नानक को एक बार सिकन्दर लोधी ने इसलिए कैद कर लिया था क्योंकि उन्होंने चमत्कार दिखाने से इन्कार कर दिया था। डाक्टर गोकुल चन्द नारंग ने लिखा है कि यह बात अधिक युक्ति संगत मालूम पड़ती है कि गुरु नानक के निर्भीक आक्षेप, जिन्हें आजकल की परिभाषा में राजद्रोह कहा जायेगा, उनके बन्दी होने के वास्तविक कारण थे।
वस्तुतः गुरु नानक निर्भय होकर मुसलमानों के कष्टकर धर्मोन्माद के विरुद्ध अपने विचार प्रकट किया करते थे और हिन्दुओं के दुःखों का रोना रोया करते थे। एक जगह उन्होंने कहा है-
‘‘समय कटार के समान है। शासक हत्यारे हैं। धर्म पंख लगाकर उड़ गया है। असत्य की अमावास्या सबके ऊपर राज्य कर रही है। सत्य का चन्द्रमा किसी को दिखाई नहीं देता।’’
चमत्कार के विषय में लेखक ने गुरु नानक का वर्णन करते हुए एक स्थान पर लिखा है-
एक धूर्त विस्मय की बातें
करता था गुरु बोले-‘‘जाव,
बड़े चमत्कारी हो तुम तो
अन्न छोड़ कर पत्थर खाव !’’
इसमें जो बात के मुँह से कहलाई है वह वास्तव में उन्हीं की कही हुई है।
इसी प्रकार गुरु तेगबहादुर ने औरंगजेब को करामात दिखाने से नाहीं कर दी थी। उनकी और औरंगजेब की बातचीत अधिकतर लेखक की कल्पनामयी है पर उसमें जो सत्य निहित है वह पूर्व का ही है।
कहते हैं, जब औरंगजेब के अत्याचार से गुरु अत्यन्त पीड़ित हुए तब उन्होंने उसे चमत्कार दिखाना मंजूर किया था। उन्होंने एक पत्र अपने गले में बाँध लिया था और कहा था कि इसे बाँधने पर गला नहीं कट सकता। किन्तु जब उनका गला कट गया और वह पत्र खोल कर देखा गया था तब उसमें यही लिखा था कि ‘सिर दिया, पर सार न दिया !’’
आगे वीर बन्दा के विषय में भी एक बार यह प्रसंग आता है। वैरागी के विषय में भी प्रसिद्ध था कि जादूगर है। इसी को सुन कर गुरु गोविन्दसिंह से प्रश्न कराकर उत्तर दिलाया गया है-
नहीं अलौकिक कुछ जगती में,
चमत्कारिणी सहसा दृष्टि;
चौंके होंगे देख प्रथम हम
चकमक की चुम्बक की सृष्टि।
लेखक ने वैरागी को योगसिद्ध अवश्य माना है, जैसा कि उसके विषय में प्रसिद्ध है। पर इसे भी लेखक अलौकिक मानने के लिए तैयार नहीं-
एक महात्मा की संगति में
साधा है मैंने कुछ योग;
अपनी ही विशेषताओं से
वंचित हैं बहुधा हम लोग।
सारांश, इसमें गुरुओं के विषय में उनकी अलौकिक बातें छोड़ कर लेखक ने उनकी महत्ता दिखाने का प्रयत्न किया है और ऐतिहासिक महापुरुषों को पौराणिक रूप नहीं दिया। आशा है, उसने यह उचित ही किया है।
पर इससे गुरु के अनुयायी यह न समझें कि लेखक ने उन्हें साधारण कोटि में रक्खा है- लेखक ने गुरु नानक के विषय में कहा है कि-
निश्चय नानक में विशेष था
उसी अकाल पुरुष का अंश।
इसी प्रकार गुरु गोविन्दसिंह को उसने ईश्वरी विभूति माना है-
इस विभूति का भी भागी था।
पाटिलपुत्र अलौकिक ओक।
और इसी विश्वास के कारण उसने उनको अधिक से अधिक अपनाने का प्रयत्न किया है। इस कारण उन बातों को भी लेखक ने छोड़ दिया है जो उसे उनके गौरव के अनुरूप नहीं मालूम हुईं।
महापुरुषों के नाम पर कितनी ही झूठी-सच्ची बातें प्रचलित हो जाया करती हैं। बहुधा लोग अपने भजनों के अन्त में जोड़ देते हैं कि-‘कहें कबीर सुनो भई साधो’। रामायण में भी कितने ही क्षेपक मिला दिये जाते हैं। पर इस सम्बन्ध में हमें सावधान रहना चाहिए। गुरु नानक के सम्बन्ध में लेखक की राय में कुछ ऐसी ही बातें प्रसिद्ध हैं। जैसे ‘‘सूर्य को जल देते देख कर गुरु का गंगाजी में अपने खेत के उद्देश्य से पानी देने लगना और यह कहना कि यदि यह पानी यहाँ से दो सौ मील मेरे खेत को नहीं पहुँच सकता तो लाखों मील दूर सूर्य को कैसे प्राप्त हो सकता है। अथवा मक्के जाकर कावे की ओर पैर करके सोने पर यह कह कर मौलवियों की आपत्ति का उत्तर देना कि यदि कावे में पैर करके सोने से खुदा की ओर पैर करके सोना पड़ता है। तो जिस ओर खुदा न हो उसी ओर मेरे पैर कर दो।’’
किसी भी धर्म के सम्बन्ध में उसके आध्यात्मिक और लौकिक रूप को न समझने वाले ऐसी कुतर्कनाएँ कर सकते हैं। पर महापुरुष कभी कुतर्कनाएँ नहीं करते। हाँ, गुरु नानक का किसी नवाब के साथ उपासना इसलिए अस्वीकार कर देना कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसका मन माया में उलझा हुआ था और शरीर से प्रणाम करता हुआ भी वह मन से कहीं घोड़े खरीद रहा था। परन्तु इस छोटी-सी पुस्तक में सब बातों का वर्णन असम्भव था।
भाई, किधर जा रहे हो तुम
अपना ओक-लोक सब छोड़।
‘‘ओक-लोक’’ कुछ क्लिष्ट होने पर भी घर-वार से अधिक अर्थ वाले एक नये मुहाविरे के रूप में रक्खा गया है।
गुरुओं के सम्बन्ध में लेखक ने यथा-सम्भव श्रद्धापूर्वक ही लिखने का प्रयत्न किया है। इसलिए पक्षकारों के सम्बन्ध में कच्छ और कृपाण के समान कड़ा, केश और कंघी का महत्त्व स्वयं न मानते हुए भी उनके विषय में युक्तियों की कल्पना की गई है। कंधे का तो स्वतन्त्र कोई अस्तित्व ही नहीं। इसलिए केशों को ही ‘‘कंघी के संगी’’ कह कर सन्तोष कर लिया गया है।
महापुरुषों के विषय में अलौकिक बातों की प्रसिद्धि स्वाभाविक है। परन्तु आश्चर्य तो इस बात का है कि गुरु प्रायः करामातों से बराबर इन्कार करते रहे; तब भी उनके सम्बन्ध में ऐसी बातों की चर्चा नहीं रुकी। महापुरुषों में विशेष शक्ति का होना लेखक को अमान्य नहीं। किन्तु इस सम्बन्ध में उसने गुरु नानक जी और गुरु तेगबहादुर जी के आदेश का पालन किया है। कहते हैं, गुरु नानक को एक बार सिकन्दर लोधी ने इसलिए कैद कर लिया था क्योंकि उन्होंने चमत्कार दिखाने से इन्कार कर दिया था। डाक्टर गोकुल चन्द नारंग ने लिखा है कि यह बात अधिक युक्ति संगत मालूम पड़ती है कि गुरु नानक के निर्भीक आक्षेप, जिन्हें आजकल की परिभाषा में राजद्रोह कहा जायेगा, उनके बन्दी होने के वास्तविक कारण थे।
वस्तुतः गुरु नानक निर्भय होकर मुसलमानों के कष्टकर धर्मोन्माद के विरुद्ध अपने विचार प्रकट किया करते थे और हिन्दुओं के दुःखों का रोना रोया करते थे। एक जगह उन्होंने कहा है-
‘‘समय कटार के समान है। शासक हत्यारे हैं। धर्म पंख लगाकर उड़ गया है। असत्य की अमावास्या सबके ऊपर राज्य कर रही है। सत्य का चन्द्रमा किसी को दिखाई नहीं देता।’’
चमत्कार के विषय में लेखक ने गुरु नानक का वर्णन करते हुए एक स्थान पर लिखा है-
एक धूर्त विस्मय की बातें
करता था गुरु बोले-‘‘जाव,
बड़े चमत्कारी हो तुम तो
अन्न छोड़ कर पत्थर खाव !’’
इसमें जो बात के मुँह से कहलाई है वह वास्तव में उन्हीं की कही हुई है।
इसी प्रकार गुरु तेगबहादुर ने औरंगजेब को करामात दिखाने से नाहीं कर दी थी। उनकी और औरंगजेब की बातचीत अधिकतर लेखक की कल्पनामयी है पर उसमें जो सत्य निहित है वह पूर्व का ही है।
कहते हैं, जब औरंगजेब के अत्याचार से गुरु अत्यन्त पीड़ित हुए तब उन्होंने उसे चमत्कार दिखाना मंजूर किया था। उन्होंने एक पत्र अपने गले में बाँध लिया था और कहा था कि इसे बाँधने पर गला नहीं कट सकता। किन्तु जब उनका गला कट गया और वह पत्र खोल कर देखा गया था तब उसमें यही लिखा था कि ‘सिर दिया, पर सार न दिया !’’
आगे वीर बन्दा के विषय में भी एक बार यह प्रसंग आता है। वैरागी के विषय में भी प्रसिद्ध था कि जादूगर है। इसी को सुन कर गुरु गोविन्दसिंह से प्रश्न कराकर उत्तर दिलाया गया है-
नहीं अलौकिक कुछ जगती में,
चमत्कारिणी सहसा दृष्टि;
चौंके होंगे देख प्रथम हम
चकमक की चुम्बक की सृष्टि।
लेखक ने वैरागी को योगसिद्ध अवश्य माना है, जैसा कि उसके विषय में प्रसिद्ध है। पर इसे भी लेखक अलौकिक मानने के लिए तैयार नहीं-
एक महात्मा की संगति में
साधा है मैंने कुछ योग;
अपनी ही विशेषताओं से
वंचित हैं बहुधा हम लोग।
सारांश, इसमें गुरुओं के विषय में उनकी अलौकिक बातें छोड़ कर लेखक ने उनकी महत्ता दिखाने का प्रयत्न किया है और ऐतिहासिक महापुरुषों को पौराणिक रूप नहीं दिया। आशा है, उसने यह उचित ही किया है।
पर इससे गुरु के अनुयायी यह न समझें कि लेखक ने उन्हें साधारण कोटि में रक्खा है- लेखक ने गुरु नानक के विषय में कहा है कि-
निश्चय नानक में विशेष था
उसी अकाल पुरुष का अंश।
इसी प्रकार गुरु गोविन्दसिंह को उसने ईश्वरी विभूति माना है-
इस विभूति का भी भागी था।
पाटिलपुत्र अलौकिक ओक।
और इसी विश्वास के कारण उसने उनको अधिक से अधिक अपनाने का प्रयत्न किया है। इस कारण उन बातों को भी लेखक ने छोड़ दिया है जो उसे उनके गौरव के अनुरूप नहीं मालूम हुईं।
महापुरुषों के नाम पर कितनी ही झूठी-सच्ची बातें प्रचलित हो जाया करती हैं। बहुधा लोग अपने भजनों के अन्त में जोड़ देते हैं कि-‘कहें कबीर सुनो भई साधो’। रामायण में भी कितने ही क्षेपक मिला दिये जाते हैं। पर इस सम्बन्ध में हमें सावधान रहना चाहिए। गुरु नानक के सम्बन्ध में लेखक की राय में कुछ ऐसी ही बातें प्रसिद्ध हैं। जैसे ‘‘सूर्य को जल देते देख कर गुरु का गंगाजी में अपने खेत के उद्देश्य से पानी देने लगना और यह कहना कि यदि यह पानी यहाँ से दो सौ मील मेरे खेत को नहीं पहुँच सकता तो लाखों मील दूर सूर्य को कैसे प्राप्त हो सकता है। अथवा मक्के जाकर कावे की ओर पैर करके सोने पर यह कह कर मौलवियों की आपत्ति का उत्तर देना कि यदि कावे में पैर करके सोने से खुदा की ओर पैर करके सोना पड़ता है। तो जिस ओर खुदा न हो उसी ओर मेरे पैर कर दो।’’
किसी भी धर्म के सम्बन्ध में उसके आध्यात्मिक और लौकिक रूप को न समझने वाले ऐसी कुतर्कनाएँ कर सकते हैं। पर महापुरुष कभी कुतर्कनाएँ नहीं करते। हाँ, गुरु नानक का किसी नवाब के साथ उपासना इसलिए अस्वीकार कर देना कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसका मन माया में उलझा हुआ था और शरीर से प्रणाम करता हुआ भी वह मन से कहीं घोड़े खरीद रहा था। परन्तु इस छोटी-सी पुस्तक में सब बातों का वर्णन असम्भव था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book