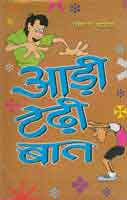|
हास्य-व्यंग्य >> आड़ी टेढ़ी बात आड़ी टेढ़ी बातरमेशचन्द्र महरोत्रा
|
355 पाठक हैं |
||||||
विसंगतियों के प्रति प्रबुद्ध वर्ग को सावधान करने और व्यवस्था को सचेत करने का अचूक अस्त्र...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
संपादकीय
कहते हैं कि टेढ़ी उंगली से ही घी निकलता है।
घी जैसी बहुमूल्य एवं पौष्टिक वस्तु को निकालने के लिए जिस प्रकार उँगली टेढ़ी
करना आवश्यक होता है उसी प्रकार समाज-सुधार जैसे उत्कृष्ट एवं पुण्य कार्य
के लिए बात टेढ़ी कहना अति आवश्यक है; क्योंकि आज के पल-प्रति पल बिगड़ते
माहौल में समाज-सुधार की कल्पना टेढ़ी खीर है।
आज हिंदी साहित्य में जब सर्वत्र व्यंग्य का ही बोलबाला है, तो उसे न अपनाकर एक नई शैली, ‘टेढ़ी बात’ का वरण निस्संदेह विचारोत्तेजक है। व्यंग्य की ही तरह ‘टेढ़ी बात’ में भी लेखक का लक्ष्य अंततोगत्वा सुधारात्मक है; परंतु दोनों में शिल्पगत अंतर है। व्यंग्य में कल्पना की छूट है, टेढ़ी बात में वह नहीं के बराबर है; व्यंग्य में स्पष्ट कथन बाधक है, टेढ़ी बात में संदर्भानुसार स्पष्ट कथन अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न करने में सहायक है; व्यंग्य में, व्याजस्तुति या व्याजनिंदा का अधिकाधिक प्रयोग होता है, टेढ़ी बात में इसके अतिरिक्त निंदनीय की खुलकर निंदा करने में कोई हिचक नहीं होती; व्यंग्य काव्य की सभी विधाओं में परिव्याप्त रहता है, जबकि टेढ़ी बात मूलतः निबंधात्मक है। व्यंग्य की अपेक्षा ‘टेढ़ी बात’ अपनाने के मूल में यह धारणा भी रही है कि जो बातें कही जा रही हैं, उन्हें कह पाना कठिन (टेढ़ा) है तथा टेढ़े-मेढ़े सवालों को हल करने के लिए टेढ़ी (वक्र) दृष्टि आवश्यक है।
‘टेढ़ी बात’ वस्तुतः अपने आस-पास की विसंगतियों के प्रति प्रबुद्ध वर्ग को सावधान करने और व्यवस्था को सचेत करने का एक ऐसा अचूक अस्त्र है, जिसकी तिरछी मार से आहत होना तयशुदा है। आचार्य कुंतक की वक्रोक्ति जिस प्रकार ध्वनि से प्रारम्भ होकर प्रकरण और प्रबंध तक रहती है उसी प्रकार डॉ. महरोत्रा की ‘टेढ़ी बात’ रचना से प्रारंभ से लेकर अंत तक अत्यंत सूक्ष्मता से काँटे से काँटा निकालने की शैली में अपना तेवर नहीं खोती।
थोड़ा कहना और ज्यादा समझना डॉ. महरोत्रा की ‘टेढ़ी बात’ की शैली है। वैसे ज्यादा कहना आसान होता है; परंतु उसकी मार उतनी तेज नहीं होती, क्योंकि कील ज्यादा नुकीली होकर ही दीवार में जल्दी घुस पाती है। देखिए— ‘जिस प्रकार सब आदमी आदमी नहीं होते उसी प्रकार सब रिसर्च स्कॉलर रिसर्च स्कॉलर नहीं होते।’
सीधे-सीधे किसी की बुराई को उजागर कर देना बहुत अच्छी बात है। पर कितने लोग हैं, जो अपनी बुराई सीधे सुनकर प्रसन्न होते हैं ? ‘टेढ़ी बात’ ऐसे प्रसंगों को बखूबी कह देती है, जो अन्यथा कठिन है—
‘सही प्रशासन चलाने के लिए नंबर दो प्रशासक को सारे चौकीदारों की हाजिरी अपने मकान पर ही लेनी पड़ती है (इससे प्रशासक का स्टेटस बढ़ता है); उसके बाद वे चौकीदार अपनी-अपनी ड्यूटी पर चाहे अगले दिन तक दिखाई न पड़ें।’
‘टेढ़ी बात’ के लेखक डॉ. महरोत्रा का इरादा बहुत नेक है। वे बीमारी बताकर मरीज की हालत में सुधार के लिए उत्सुक हैं; क्योंकि उनके मन में समाज के हित के प्रति सच्चा लगाव है। इसी कारण हर छोटी-बड़ी अव्यवस्था से वे पीड़ित-चिंतित हैं—
‘एक युग पहले हमारे एक रहमदिल कुल-प्रबंधक ने सड़कें बनवाने के लिए किसी ठेकेदार से दर्जनों जगह किनारे-किनारे गिट्टी-पत्थर डलवा दिए थे। अब वे सारे कैंपस में सच्चे समाजवादी भाव से फैल गए हैं—सड़कों पर, मैदानों में, मकानों के दरवाजों तक। इससे एक जबरदस्त लाभ हो गया है कि कुत्तों को भगाने के लिए एक पत्थर उठाने के लिए एक कदम से ज्यादा कहीं नहीं चलना पड़ता।’
इस संकलन में आधी से अधिक रचनाएँ विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। क्यों ? ‘शिक्षा राष्ट्र की रीढ़ है और शिक्षक राष्ट्रनिर्माता हैं’-इस उक्ति के आधार पर यह कहना सर्वथा उचित है कि समाज में बहुआयामी दुर्व्यवस्था की वजह शिक्षा ही है। फिर विश्वविद्यालय शिक्षा का अंतिम पड़ाव होने के कारण तथा विश्वविद्यालयीन सेवा में अपना जीवन समर्पित करने के कारण जाहिर है कि डॉ. महरोत्रा की सूक्ष्म दृष्टि जितनी शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी आदि की जड़ों तक पहुँच सकती है उतनी अन्य व्यक्ति की कदाचित् न जा पाए—
‘ ‘सामान्य बोध’ का यह अनिवार्य प्रश्नपत्र छात्रों के सामान्य ज्ञान को सुदृढ़ बनाने के लिए रहता है। यद्यपि वे इसे ‘बोध’ की जगह ‘बोझ’ मानते हैं, क्योंकि इसकी पढ़ाई की व्यवस्था ‘नहीं के बराबर’ रहती है, पर वे गेस-पेपर या गाइड के जरिए प्रायः परीक्षा के पूर्व, दो-तीन दिनों के गैप में ही, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं।’
‘अपने द्वारा सेट किए गए प्रश्नपत्र को आउट करने का प्रति प्रश्न रेट तय रहता है। यदि आप मॉडरेटर हैं तो सारे प्रश्नपत्र आपकी मुट्ठी में हैं, अपनी हस्ती पहचानिए। परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का एक-एक अंक सच्चे मोती की कीमत का होता है। उसके बाद टैबुलेशन, स्क्रुटनी और रीवैल्यूएशन के समय उसका मूल्य बढ़कर हीरों के समान हो जाता है।’
‘छात्र कहता है कि उसने ‘सही और बहुत अच्छा’ लिखा है। वे भी कहते हैं कि छात्र ने जरूरत से ज्यादा सही और अच्छा लिखा है। छात्र कहता है कि उसे इतने प्रतिशत अंक मिलने चाहिए। पुनर्मूल्यांकन करवाने वाले भी कहते हैं कि छात्र तो उतने प्रतिशत से कम अंक नहीं मिलने चाहिए। छात्र की बात को वे नहीं काट सकते, क्योंकि उसे काटने के लिए उसकी कॉपी को पढ़ना जरूरी होता है।’
शिक्षा के अतिरिक्त जीवन के विविध पक्षों पर भी लेखक की दृष्टि उतनी ही सूक्ष्म है। एक मध्यम वर्गीय आदमी की हैसियत से आस्पताल, पोस्ट ऑफिस, बैंक, टेलीफोन, बिजली, राशन की दुकान, आयकर, नगर निगम, रेलवे, पुलिस, रेडियो, दूरदर्शन, शासन, प्रशासन, धर्म, अध्यात्म, साहित्य आदि की राजनीति की समझ हर एक को है; पर उनमें व्याप्त अराजकता और मनमानी को चुपचाप सह लेना और भगवद्-भजन करना कदाचित् ईश्वर को धोखा देना है—
‘वे यह मानकर चलते हैं कि उनकी रक्षा का पूरा दायित्व देवी-देवताओं पर है; उनके सारे (अंध) विश्वासों के सामने झुककर उन्हें परमधाम तक पहुँचाने का ठेका मेले के आयोजकों पर है।’
अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए होता है; परंतु सरकारी अस्पतालों की हालत आज कैसी है, यह किसी से छिपा नहीं है। ऐसे ही एक अस्पताल की तथाकथा लेखक के शब्दों में इस प्रकार है—
‘किसी मरीज के इलाज के मामले में जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तब कहा जाता है कि अब दवा से नहीं, दुआ से काम चलेगा। डॉक्टरों से ऐसा जवाब (कि अब ‘दुआ’ करो) काफी जल्दी मिलनेवाला एक अस्पताल है ‘डी.के. ; अर्थात् ‘दुआ करो अस्पताल’।’
‘किसी समय पोस्ट ऑफिस सरकारी विभागों में सबसे ज्यादा अच्छा विभाग था, पर अब पोस्ट ऑफिस भी अन्य ‘नाम कमानेवाले’ विभागों के समान अभावों की कहानी लिखने में माहिर हो चले हैं। कहीं विद्ड्रॉवल के जरिए राशि का अभाव है, कहीं चिल्लर का अभाव है; कहीं डाक सामग्री का अभाव है, कहीं विशेष उपकरणों का अभाव; कहीं स्पेस का अभाव है, कहीं स्टाफ का अभाव है; कहीं कार्य-कुशलता का अभाव है, कहीं शिष्टाचार का आभाव है।’
रेलवे-टाइम किसी जमाने में मशहूर रहा है; पर आज की स्थिति क्या है, लेखक की लेखनी इसे मूर्त्त कर देने में इस प्रकार सफल है—
‘रेलवेवाले अब अपनी घड़ियाँ इसलिए सही नहीं रखते हैं कि इनकी बदौलत न जाने कब किसकी घड़ी आ जाए। जब हर रोज एक-दो रेल एक्सीडेंट करने हैं तो कहाँ तक घड़ी देखकर करें।’
आज के अर्थ-प्रधान युग में बैंक की अहमियत को कौन नकार सकता है ! वहाँ ग्राहकों को मिलने वाली सुविधाएँ भी अपार हैं; नमूने के बतौर--‘जब-जब आप बैंकों से नोटों की गड्डी लाते हैं—चाहे दस के, चाहे सौ के नोटों की—तब-तब आपको घर आकर क्या करना पड़ता है, यह छिपाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अधिकतर भुक्तभोगियों को एक सा ही कलियुग झेलना पड़ रहा है। हाँ, वित्तमंत्री आदि को कभी पता नहीं चल पाता कि उन गड्डियों की कितनी प्रगतिशील हालत रही है।’
स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा तरक्की हमारे देश में यदि किसी विभाग ने की है तो वह है पुलिस विभाग ! ‘पुलिसवालों का क्या काम है ? तन-मन-धन से खुद अपनी सुरक्षा करना। आप भी अपनी सुरक्षा स्वयं ही कीजिए, विशेषकर पुलिसवालों से। वरना यदि आपने किसी काम से उनसे संपर्क साधा तो आप आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकार के संकट में पड़ जाएँगे।’ और ‘यदि आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपके लिए न्याय के दरवाजे सदा खुले हैं। न्याय पाने के लिए ‘न्याय के घर’ (न्याय के आलय) को अपना ही घर समझकर वहाँ खूब जाना-आना करते रहिए। अपने घर में क्या संकोच !’
विज्ञान और तकनीकी के विकास ने आधुनिक मानव को जितना अधिक सुविधाभोगी बना दिया है उतना ही अधिक कामचोर भी। फलस्वरूप लोग ऐसे धंधे की तलाश में हैं जिसमें कुछ भी न करना पड़े। ऐसा ही एक धंधा है नेतागिरी। ‘लोग नेता क्यों बनना चाहते हैं ? इसलिए कि उसमें किसी भी दुकान को चलाने का तुलना में कम मेहनत करनी पड़ती है। दूसरे इसलिए कि कोई अन्य धंधा शुरू करने के लिए पूँजी चाहिए, जबकि नेतागिरी खाली जेब से भी शुरू हो सकती है। अन्य धंधों में रुपये जाते भी हैं और आते भी हैं, पर नेतागिरी में बस आते-ही-आते हैं।’ इसके अतिरिक्त ‘नेतागिरी कोई नौकरी न होकर धंधा इसलिए है कि इसमें कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती, जिसका कारण यह है कि नेता बनते ही आदमी हर दिन अधिकाधिक जवान होता चला जाता है।’
हमारे दैनंदिन जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं, जहाँ सिवाय गाली के और कुछ नहीं निकल सकता। ‘टेढ़ी बात’ में ऐसे प्रसंग यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं, उदाहरणार्थ—
‘या तो ट्यूब-रॉडें अचानक गायब कर दी जाती हैं या वे चार दिन जलने के बाद ही फकर-फकर करने लगती हैं। डुप्लीकेट माल बनाने में हमारे देश ने काफी तरक्की की है। ‘खरीदो’ साठ रुपयेवाली, लगाओ बीस रुपयेवाली। जय गुरुदेव !’
‘अमुक पूरा जिला साक्षर हो गया। वाह, सबको अपना-अपना नाम लिखना आ गया। चमत्कार ! खर्च सिर्फ कुछ करोड़ रुपया आया, जिसमें नब्बे प्रतिशत राशि की ऊपर से नीचे तक की उन समितियों और टीमों ने जुगाली कर डाली, जिनके कंधों पर इस भारी दायित्व का जुआ रखा गया।’
‘प्लेटफॉर्म चलने-फिरनेवाले ठेलों के बिना नहीं चलता। ये ठेले खुले साँड़ के समान घूमते रहते हैं। इनसे घायल होने से बचने के लिए प्रतीक्षार्थियों को जल्दी-जल्दी इधर-उधर होना पड़ता है, जिससे उनका आलस्य दूर होता है और नींद नहीं आती।’
‘टेढ़ी बात’ के लेखक डॉ. महरोत्रा एक ओर कुसुम से भी अधिक कोमल हैं तो दूसरी ओर वज्र से भी अधिक कठोर। कोमलता ऐसी कि दूसरों के दुःख से वे द्रवित हुए बिना नहीं रहते और कठोरता ऐसी कि खुद तक को नहीं बख्शते। ‘टेढ़ी बात’ की रचना-प्रक्रिया में ये दोनों ही छोर सर्वत्र विद्यमान हैं। उन्हें समाज-सापेक्ष (समाज-निरपेक्ष नहीं) व्यक्तिगत हित इष्ट है, जिससे वे समाज के निरंतर गिरते हुए मूल्यों के प्रति करुणार्द्र हो उठते हैं और इन गिरते हुए मूल्यों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या व्यवस्था के प्रति उनका आक्रोश औपचारिकताओं की सारी क्रत्रिम सीमाएँ तोड़कर मुखर हो उठता है—
‘नगर में जगह-जगह से कूड़े के ढेर जान-बूझकर नहीं हटाए जाते, क्योंकि यदि वहाँ सफाई हो गई तो राह चलते लोगों को सफाई करनेवाले रामलाल और श्यामलाल की याद कैसे आएगी। अपना अस्तित्व सिद्ध करने और अपनी जरूरत महसूस कराने के लिए पेंडिंग काम सदा दीखना चाहिए। यदि आपने अपना काम निबटा डाला तो लोगों को लगेगा आप खाली पड़े हैं।’
स्पष्टवादिता व्यक्ति की नैतिकता और निर्भीरता की परिणति है और ‘टेढ़ी बात’ में यह स्पष्टवादिता और भी ‘टेढ़ी’ होकर उसके तेवर पर धार चढ़ा देती है—
‘ऑडिटर लोग आर्थिक पहलुओं के बारे में बेहद अक्लमंद होते हैं। उन सबको वित्तमंत्री बना दिया जाना चाहिए। वे लाखों रुपयों का लेखा तीन मिनट में समायोजित करने विद्वता और क्षमता रखते हैं। बस, उन्हें एक मोटा-सा ‘टुकड़ा चाहिए। टुकड़े के संकटमोटन दर्शन होते ही उनकी बुद्धि सारे नियमों का श्राद्ध करने की योग्यता अर्जित कर लेती है।’
इसे यदि कोई ‘निंदा’ कहता है तो लेखक ‘निंदक’ कहलाने को भी तैयार है। लेखक के ही शब्दों में-‘निंदक नियरे राखिए’ के हिसाब से हम ‘निंदक’ कहलाने को तैयार हैं। वस्तुस्थिति यह है कि खुलकर लिखनेवाला व्यक्ति केवल उनके लिए ‘निंदक’ होता है, जिनकी वह पोल खोल रहा होता है। अन्य लाखों लोगों के लिए वह ‘निंदित’ का प्रचारक, प्रकाशक और सुधारक होता है। वह सत्यभाषी होता है।’
‘टेढ़ी बात’ के लेखक ने एक नई शैली अपनाकर अपना सारा आक्रोश निकाल देने की अच्छी तरकीब निकाली है। वह है ‘मैं’ की शैली। इससे उक्ति की वक्रता द्विगुणित हो गई है—
‘मैं रबड़ीपारा विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ। कुलपति बनने के पहले की मेरी हर भूख और अतृप्त वासना आजकल पूरी हो रही है—लंबे-चौड़े बँगले की, नौकर-चौकरों की, कारों-ड्राइवरों की, लाखों में खेलने की, अखबारों में नाम और फोटो की भयंकर छपास की, जबरदस्ती अपनी इज्जत कराने और जब-तब दूसरों की बेइज्जती करने की, अड़ियल टट्टू बनकर हुक्म चलाने की और सिद्धांतों का थोथा डंका पीटने की।’
व्यंग्य के साथ हास्य की कल्पना टेढ़ी है, क्योंकि व्यंग्य के मूल में करुणा होने की वजह से हास्य उससे काफी दूर जा छिटकता है; परंतु यह भी सच है कि हास्य के व्यतिरेक से करुणा और भी गहरी हो जाती है। हास्य अश्लीलता या फूहड़पन से भी उपजता है, बेतुकी हरकत से भी उपजता है; परंतु सहज-शिष्ट हास्य ही वह रस है, जिसका आनंद सभी बेहिचक ले सकते हैं तथा जो कभी बासी नहीं होता। लीजिए हास्य-व्यंग्य का मजा—
‘कुछ लोग कह रहे थे कि जिस प्रकार अन्य शादियों में पूछा जाता है कि आपने खा लिया क्या, उस प्रकार इसमें लोग पूछ रहे थे कि आपको कुछ मिला क्या ?’
‘वे बेचारे देश-प्रेम की खातिर बार-बार घर-बार छोड़कर राजधानी चले जाते हैं और वहाँ देश-प्रेम करते हुए नजर आते हैं। उनकी आमदनी का जरिया देश-प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। कृपा करके आप भी सुबह-शाम देश-प्रेम किया कीजिए।’
ऐसे ही रोज के टेढ़े-मेढ़े सवालों को हल करने के लिहाज से ‘टेढ़ी बात’ की रचना हुई है, जिसमें ‘कल्पना’ का स्थान केवल उतना ही है जितना ‘सत्य’ को ‘साहित्य’ बनाने के लिए आवश्यक है। प्रत्येक रचना में लेखक की शोधी प्रवृत्ति तथा यथाशक्ति-यथासंभव ऐक्यूरेट होने की ललक समस्या या स्थिति की अनेकानेक परतें खोलने में साधक रही है।
साहित्य भाषा की कला है और भाषा की कला में डॉ. महरोत्रा खूब माहिर हैं—न कहीं एक कॉमा अधिक और न कहीं एक फुलस्टॉप कम। भाषा के यथेष्ट प्रयोग के लिए शब्दों की आत्मा में प्रवेश करके उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, वह यदि एक ओर साहित्यानुरागियों को रसाप्लावित करता चलता है तो दूसरी ओर भाषा-प्रेमियों को व्याकरण एवं प्रयोग के दृष्टांत बताता चलता है। डॉ. महरोत्रा की सुदीर्घकालीन हिंदी-सेवा से भाषा-अधिगम के लिए पुष्कल सामग्री पदे-पदे मिलती है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कुछ ऐसे स्पेलिंग और लिपि-चिह्न विकसित किए हैं, जो हिंदी की प्रकृति के लिए इष्ट और तर्कसम्मत होने के कारण विविध हिंदी-सेवियों, संस्थाओं और प्रेसों आदि को भी मान्य हैं।
कुल मिलाकर डॉ. महरोत्रा की ‘टेढ़ी बात’ कहीं दीयों के तले अँधेरे को उजागर करती है तो कहीं जन-मानस को अपने कर्तव्यों और दायित्वों का बोध कराती चलती है; कहीं वह गलतफहमी के शिकार लोगों को असलियत से वाकिफ कराती चलती है तो कहीं गलत लोगों को सही राह पर चलना सिखाती चलती है। वह एक ऐसा आइना है, जिसमें हमारे समाज की सच्ची तसवीर दिखाई देती है, जिसे देखकर एक सच्चे मानव में करुणा उपजती है। यह करुणा ही वस्तुतः लेखनी की छटपटाहट बनकर ‘टेढ़ी बात’ के रूप में ढल गई है।
साहित्य में ‘बासी’ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, साहित्य का ‘सत्य’ और अधिक मूल्यवान और प्रासंगिक होने लगता है। गनीमत है, यहाँ पुराने मॉडल का स्थान नए मॉडल नहीं ले पाते, अन्यथा कालीदास या शेक्सपीयर का नाम भी नहीं रह पाता।
हाँ, रुचि बदलती है मनुष्य की, जिससे वह पुराने में कुछ जोड़ता और उससे कुछ घटाता चलता है। ‘टेढ़ी बात’ को ‘आड़ी-टेढ़ी बात’ बनकर आने में कुछ-न-कुछ परिवर्तन-परिवर्धन तो स्वीकारना ही पड़ा है—मात्रा में भी और आस्वाद में भी। केवल शीर्षक बदल देना समाज के साथ न्याय कदापि नहीं है।
‘टेढ़ी बात’ के ‘आड़ी-टेढ़ी बात’ रूपांतरण में ‘आड़ी-टेढ़ी’ विश्लेषण गतिसूचक है—रचना की दृष्टि से और अर्थ ग्रहण की दृष्टि से, अर्थात् जब जैसी स्थिति हो, वैसा ही आड़ा-टेढ़ापन आवश्यक है। इन रचनाओं में केवल रोग नहीं, उनका उपचार भी है—कहीं सीधे ढंग से तो कहीं आड़े-टेढ़े ढंग से। देश के हित में केवल उपदेश काम नहीं आते, अतः डॉ. महरोत्रा ने कहीं-कहीं संदेश और निर्देश भी दिए हैं। साधी-सादी बातों में (हो सकता है) व्यंग्य की धार न मिले, परंतु उनसे अभीष्ट-सिद्धि में अद्भुत सहायता मिलती है—स्पष्टवादिता के कारण कंट्रास्ट के रूप में। वैसे भी किसी संकलन की सभी रचनाएँ एक ही तेवर की शायद ही होती हों। हिमालय की सारी चोटियाँ भी एवरेस्ट कहाँ हुआ करती हैं, तथापि पूरी श्रेणी हिमालय ही कहलाती है।
आज हिंदी साहित्य में जब सर्वत्र व्यंग्य का ही बोलबाला है, तो उसे न अपनाकर एक नई शैली, ‘टेढ़ी बात’ का वरण निस्संदेह विचारोत्तेजक है। व्यंग्य की ही तरह ‘टेढ़ी बात’ में भी लेखक का लक्ष्य अंततोगत्वा सुधारात्मक है; परंतु दोनों में शिल्पगत अंतर है। व्यंग्य में कल्पना की छूट है, टेढ़ी बात में वह नहीं के बराबर है; व्यंग्य में स्पष्ट कथन बाधक है, टेढ़ी बात में संदर्भानुसार स्पष्ट कथन अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न करने में सहायक है; व्यंग्य में, व्याजस्तुति या व्याजनिंदा का अधिकाधिक प्रयोग होता है, टेढ़ी बात में इसके अतिरिक्त निंदनीय की खुलकर निंदा करने में कोई हिचक नहीं होती; व्यंग्य काव्य की सभी विधाओं में परिव्याप्त रहता है, जबकि टेढ़ी बात मूलतः निबंधात्मक है। व्यंग्य की अपेक्षा ‘टेढ़ी बात’ अपनाने के मूल में यह धारणा भी रही है कि जो बातें कही जा रही हैं, उन्हें कह पाना कठिन (टेढ़ा) है तथा टेढ़े-मेढ़े सवालों को हल करने के लिए टेढ़ी (वक्र) दृष्टि आवश्यक है।
‘टेढ़ी बात’ वस्तुतः अपने आस-पास की विसंगतियों के प्रति प्रबुद्ध वर्ग को सावधान करने और व्यवस्था को सचेत करने का एक ऐसा अचूक अस्त्र है, जिसकी तिरछी मार से आहत होना तयशुदा है। आचार्य कुंतक की वक्रोक्ति जिस प्रकार ध्वनि से प्रारम्भ होकर प्रकरण और प्रबंध तक रहती है उसी प्रकार डॉ. महरोत्रा की ‘टेढ़ी बात’ रचना से प्रारंभ से लेकर अंत तक अत्यंत सूक्ष्मता से काँटे से काँटा निकालने की शैली में अपना तेवर नहीं खोती।
थोड़ा कहना और ज्यादा समझना डॉ. महरोत्रा की ‘टेढ़ी बात’ की शैली है। वैसे ज्यादा कहना आसान होता है; परंतु उसकी मार उतनी तेज नहीं होती, क्योंकि कील ज्यादा नुकीली होकर ही दीवार में जल्दी घुस पाती है। देखिए— ‘जिस प्रकार सब आदमी आदमी नहीं होते उसी प्रकार सब रिसर्च स्कॉलर रिसर्च स्कॉलर नहीं होते।’
सीधे-सीधे किसी की बुराई को उजागर कर देना बहुत अच्छी बात है। पर कितने लोग हैं, जो अपनी बुराई सीधे सुनकर प्रसन्न होते हैं ? ‘टेढ़ी बात’ ऐसे प्रसंगों को बखूबी कह देती है, जो अन्यथा कठिन है—
‘सही प्रशासन चलाने के लिए नंबर दो प्रशासक को सारे चौकीदारों की हाजिरी अपने मकान पर ही लेनी पड़ती है (इससे प्रशासक का स्टेटस बढ़ता है); उसके बाद वे चौकीदार अपनी-अपनी ड्यूटी पर चाहे अगले दिन तक दिखाई न पड़ें।’
‘टेढ़ी बात’ के लेखक डॉ. महरोत्रा का इरादा बहुत नेक है। वे बीमारी बताकर मरीज की हालत में सुधार के लिए उत्सुक हैं; क्योंकि उनके मन में समाज के हित के प्रति सच्चा लगाव है। इसी कारण हर छोटी-बड़ी अव्यवस्था से वे पीड़ित-चिंतित हैं—
‘एक युग पहले हमारे एक रहमदिल कुल-प्रबंधक ने सड़कें बनवाने के लिए किसी ठेकेदार से दर्जनों जगह किनारे-किनारे गिट्टी-पत्थर डलवा दिए थे। अब वे सारे कैंपस में सच्चे समाजवादी भाव से फैल गए हैं—सड़कों पर, मैदानों में, मकानों के दरवाजों तक। इससे एक जबरदस्त लाभ हो गया है कि कुत्तों को भगाने के लिए एक पत्थर उठाने के लिए एक कदम से ज्यादा कहीं नहीं चलना पड़ता।’
इस संकलन में आधी से अधिक रचनाएँ विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। क्यों ? ‘शिक्षा राष्ट्र की रीढ़ है और शिक्षक राष्ट्रनिर्माता हैं’-इस उक्ति के आधार पर यह कहना सर्वथा उचित है कि समाज में बहुआयामी दुर्व्यवस्था की वजह शिक्षा ही है। फिर विश्वविद्यालय शिक्षा का अंतिम पड़ाव होने के कारण तथा विश्वविद्यालयीन सेवा में अपना जीवन समर्पित करने के कारण जाहिर है कि डॉ. महरोत्रा की सूक्ष्म दृष्टि जितनी शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी आदि की जड़ों तक पहुँच सकती है उतनी अन्य व्यक्ति की कदाचित् न जा पाए—
‘ ‘सामान्य बोध’ का यह अनिवार्य प्रश्नपत्र छात्रों के सामान्य ज्ञान को सुदृढ़ बनाने के लिए रहता है। यद्यपि वे इसे ‘बोध’ की जगह ‘बोझ’ मानते हैं, क्योंकि इसकी पढ़ाई की व्यवस्था ‘नहीं के बराबर’ रहती है, पर वे गेस-पेपर या गाइड के जरिए प्रायः परीक्षा के पूर्व, दो-तीन दिनों के गैप में ही, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं।’
‘अपने द्वारा सेट किए गए प्रश्नपत्र को आउट करने का प्रति प्रश्न रेट तय रहता है। यदि आप मॉडरेटर हैं तो सारे प्रश्नपत्र आपकी मुट्ठी में हैं, अपनी हस्ती पहचानिए। परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का एक-एक अंक सच्चे मोती की कीमत का होता है। उसके बाद टैबुलेशन, स्क्रुटनी और रीवैल्यूएशन के समय उसका मूल्य बढ़कर हीरों के समान हो जाता है।’
‘छात्र कहता है कि उसने ‘सही और बहुत अच्छा’ लिखा है। वे भी कहते हैं कि छात्र ने जरूरत से ज्यादा सही और अच्छा लिखा है। छात्र कहता है कि उसे इतने प्रतिशत अंक मिलने चाहिए। पुनर्मूल्यांकन करवाने वाले भी कहते हैं कि छात्र तो उतने प्रतिशत से कम अंक नहीं मिलने चाहिए। छात्र की बात को वे नहीं काट सकते, क्योंकि उसे काटने के लिए उसकी कॉपी को पढ़ना जरूरी होता है।’
शिक्षा के अतिरिक्त जीवन के विविध पक्षों पर भी लेखक की दृष्टि उतनी ही सूक्ष्म है। एक मध्यम वर्गीय आदमी की हैसियत से आस्पताल, पोस्ट ऑफिस, बैंक, टेलीफोन, बिजली, राशन की दुकान, आयकर, नगर निगम, रेलवे, पुलिस, रेडियो, दूरदर्शन, शासन, प्रशासन, धर्म, अध्यात्म, साहित्य आदि की राजनीति की समझ हर एक को है; पर उनमें व्याप्त अराजकता और मनमानी को चुपचाप सह लेना और भगवद्-भजन करना कदाचित् ईश्वर को धोखा देना है—
‘वे यह मानकर चलते हैं कि उनकी रक्षा का पूरा दायित्व देवी-देवताओं पर है; उनके सारे (अंध) विश्वासों के सामने झुककर उन्हें परमधाम तक पहुँचाने का ठेका मेले के आयोजकों पर है।’
अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए होता है; परंतु सरकारी अस्पतालों की हालत आज कैसी है, यह किसी से छिपा नहीं है। ऐसे ही एक अस्पताल की तथाकथा लेखक के शब्दों में इस प्रकार है—
‘किसी मरीज के इलाज के मामले में जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तब कहा जाता है कि अब दवा से नहीं, दुआ से काम चलेगा। डॉक्टरों से ऐसा जवाब (कि अब ‘दुआ’ करो) काफी जल्दी मिलनेवाला एक अस्पताल है ‘डी.के. ; अर्थात् ‘दुआ करो अस्पताल’।’
‘किसी समय पोस्ट ऑफिस सरकारी विभागों में सबसे ज्यादा अच्छा विभाग था, पर अब पोस्ट ऑफिस भी अन्य ‘नाम कमानेवाले’ विभागों के समान अभावों की कहानी लिखने में माहिर हो चले हैं। कहीं विद्ड्रॉवल के जरिए राशि का अभाव है, कहीं चिल्लर का अभाव है; कहीं डाक सामग्री का अभाव है, कहीं विशेष उपकरणों का अभाव; कहीं स्पेस का अभाव है, कहीं स्टाफ का अभाव है; कहीं कार्य-कुशलता का अभाव है, कहीं शिष्टाचार का आभाव है।’
रेलवे-टाइम किसी जमाने में मशहूर रहा है; पर आज की स्थिति क्या है, लेखक की लेखनी इसे मूर्त्त कर देने में इस प्रकार सफल है—
‘रेलवेवाले अब अपनी घड़ियाँ इसलिए सही नहीं रखते हैं कि इनकी बदौलत न जाने कब किसकी घड़ी आ जाए। जब हर रोज एक-दो रेल एक्सीडेंट करने हैं तो कहाँ तक घड़ी देखकर करें।’
आज के अर्थ-प्रधान युग में बैंक की अहमियत को कौन नकार सकता है ! वहाँ ग्राहकों को मिलने वाली सुविधाएँ भी अपार हैं; नमूने के बतौर--‘जब-जब आप बैंकों से नोटों की गड्डी लाते हैं—चाहे दस के, चाहे सौ के नोटों की—तब-तब आपको घर आकर क्या करना पड़ता है, यह छिपाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अधिकतर भुक्तभोगियों को एक सा ही कलियुग झेलना पड़ रहा है। हाँ, वित्तमंत्री आदि को कभी पता नहीं चल पाता कि उन गड्डियों की कितनी प्रगतिशील हालत रही है।’
स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा तरक्की हमारे देश में यदि किसी विभाग ने की है तो वह है पुलिस विभाग ! ‘पुलिसवालों का क्या काम है ? तन-मन-धन से खुद अपनी सुरक्षा करना। आप भी अपनी सुरक्षा स्वयं ही कीजिए, विशेषकर पुलिसवालों से। वरना यदि आपने किसी काम से उनसे संपर्क साधा तो आप आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकार के संकट में पड़ जाएँगे।’ और ‘यदि आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपके लिए न्याय के दरवाजे सदा खुले हैं। न्याय पाने के लिए ‘न्याय के घर’ (न्याय के आलय) को अपना ही घर समझकर वहाँ खूब जाना-आना करते रहिए। अपने घर में क्या संकोच !’
विज्ञान और तकनीकी के विकास ने आधुनिक मानव को जितना अधिक सुविधाभोगी बना दिया है उतना ही अधिक कामचोर भी। फलस्वरूप लोग ऐसे धंधे की तलाश में हैं जिसमें कुछ भी न करना पड़े। ऐसा ही एक धंधा है नेतागिरी। ‘लोग नेता क्यों बनना चाहते हैं ? इसलिए कि उसमें किसी भी दुकान को चलाने का तुलना में कम मेहनत करनी पड़ती है। दूसरे इसलिए कि कोई अन्य धंधा शुरू करने के लिए पूँजी चाहिए, जबकि नेतागिरी खाली जेब से भी शुरू हो सकती है। अन्य धंधों में रुपये जाते भी हैं और आते भी हैं, पर नेतागिरी में बस आते-ही-आते हैं।’ इसके अतिरिक्त ‘नेतागिरी कोई नौकरी न होकर धंधा इसलिए है कि इसमें कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती, जिसका कारण यह है कि नेता बनते ही आदमी हर दिन अधिकाधिक जवान होता चला जाता है।’
हमारे दैनंदिन जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं, जहाँ सिवाय गाली के और कुछ नहीं निकल सकता। ‘टेढ़ी बात’ में ऐसे प्रसंग यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं, उदाहरणार्थ—
‘या तो ट्यूब-रॉडें अचानक गायब कर दी जाती हैं या वे चार दिन जलने के बाद ही फकर-फकर करने लगती हैं। डुप्लीकेट माल बनाने में हमारे देश ने काफी तरक्की की है। ‘खरीदो’ साठ रुपयेवाली, लगाओ बीस रुपयेवाली। जय गुरुदेव !’
‘अमुक पूरा जिला साक्षर हो गया। वाह, सबको अपना-अपना नाम लिखना आ गया। चमत्कार ! खर्च सिर्फ कुछ करोड़ रुपया आया, जिसमें नब्बे प्रतिशत राशि की ऊपर से नीचे तक की उन समितियों और टीमों ने जुगाली कर डाली, जिनके कंधों पर इस भारी दायित्व का जुआ रखा गया।’
‘प्लेटफॉर्म चलने-फिरनेवाले ठेलों के बिना नहीं चलता। ये ठेले खुले साँड़ के समान घूमते रहते हैं। इनसे घायल होने से बचने के लिए प्रतीक्षार्थियों को जल्दी-जल्दी इधर-उधर होना पड़ता है, जिससे उनका आलस्य दूर होता है और नींद नहीं आती।’
‘टेढ़ी बात’ के लेखक डॉ. महरोत्रा एक ओर कुसुम से भी अधिक कोमल हैं तो दूसरी ओर वज्र से भी अधिक कठोर। कोमलता ऐसी कि दूसरों के दुःख से वे द्रवित हुए बिना नहीं रहते और कठोरता ऐसी कि खुद तक को नहीं बख्शते। ‘टेढ़ी बात’ की रचना-प्रक्रिया में ये दोनों ही छोर सर्वत्र विद्यमान हैं। उन्हें समाज-सापेक्ष (समाज-निरपेक्ष नहीं) व्यक्तिगत हित इष्ट है, जिससे वे समाज के निरंतर गिरते हुए मूल्यों के प्रति करुणार्द्र हो उठते हैं और इन गिरते हुए मूल्यों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या व्यवस्था के प्रति उनका आक्रोश औपचारिकताओं की सारी क्रत्रिम सीमाएँ तोड़कर मुखर हो उठता है—
‘नगर में जगह-जगह से कूड़े के ढेर जान-बूझकर नहीं हटाए जाते, क्योंकि यदि वहाँ सफाई हो गई तो राह चलते लोगों को सफाई करनेवाले रामलाल और श्यामलाल की याद कैसे आएगी। अपना अस्तित्व सिद्ध करने और अपनी जरूरत महसूस कराने के लिए पेंडिंग काम सदा दीखना चाहिए। यदि आपने अपना काम निबटा डाला तो लोगों को लगेगा आप खाली पड़े हैं।’
स्पष्टवादिता व्यक्ति की नैतिकता और निर्भीरता की परिणति है और ‘टेढ़ी बात’ में यह स्पष्टवादिता और भी ‘टेढ़ी’ होकर उसके तेवर पर धार चढ़ा देती है—
‘ऑडिटर लोग आर्थिक पहलुओं के बारे में बेहद अक्लमंद होते हैं। उन सबको वित्तमंत्री बना दिया जाना चाहिए। वे लाखों रुपयों का लेखा तीन मिनट में समायोजित करने विद्वता और क्षमता रखते हैं। बस, उन्हें एक मोटा-सा ‘टुकड़ा चाहिए। टुकड़े के संकटमोटन दर्शन होते ही उनकी बुद्धि सारे नियमों का श्राद्ध करने की योग्यता अर्जित कर लेती है।’
इसे यदि कोई ‘निंदा’ कहता है तो लेखक ‘निंदक’ कहलाने को भी तैयार है। लेखक के ही शब्दों में-‘निंदक नियरे राखिए’ के हिसाब से हम ‘निंदक’ कहलाने को तैयार हैं। वस्तुस्थिति यह है कि खुलकर लिखनेवाला व्यक्ति केवल उनके लिए ‘निंदक’ होता है, जिनकी वह पोल खोल रहा होता है। अन्य लाखों लोगों के लिए वह ‘निंदित’ का प्रचारक, प्रकाशक और सुधारक होता है। वह सत्यभाषी होता है।’
‘टेढ़ी बात’ के लेखक ने एक नई शैली अपनाकर अपना सारा आक्रोश निकाल देने की अच्छी तरकीब निकाली है। वह है ‘मैं’ की शैली। इससे उक्ति की वक्रता द्विगुणित हो गई है—
‘मैं रबड़ीपारा विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ। कुलपति बनने के पहले की मेरी हर भूख और अतृप्त वासना आजकल पूरी हो रही है—लंबे-चौड़े बँगले की, नौकर-चौकरों की, कारों-ड्राइवरों की, लाखों में खेलने की, अखबारों में नाम और फोटो की भयंकर छपास की, जबरदस्ती अपनी इज्जत कराने और जब-तब दूसरों की बेइज्जती करने की, अड़ियल टट्टू बनकर हुक्म चलाने की और सिद्धांतों का थोथा डंका पीटने की।’
व्यंग्य के साथ हास्य की कल्पना टेढ़ी है, क्योंकि व्यंग्य के मूल में करुणा होने की वजह से हास्य उससे काफी दूर जा छिटकता है; परंतु यह भी सच है कि हास्य के व्यतिरेक से करुणा और भी गहरी हो जाती है। हास्य अश्लीलता या फूहड़पन से भी उपजता है, बेतुकी हरकत से भी उपजता है; परंतु सहज-शिष्ट हास्य ही वह रस है, जिसका आनंद सभी बेहिचक ले सकते हैं तथा जो कभी बासी नहीं होता। लीजिए हास्य-व्यंग्य का मजा—
‘कुछ लोग कह रहे थे कि जिस प्रकार अन्य शादियों में पूछा जाता है कि आपने खा लिया क्या, उस प्रकार इसमें लोग पूछ रहे थे कि आपको कुछ मिला क्या ?’
‘वे बेचारे देश-प्रेम की खातिर बार-बार घर-बार छोड़कर राजधानी चले जाते हैं और वहाँ देश-प्रेम करते हुए नजर आते हैं। उनकी आमदनी का जरिया देश-प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। कृपा करके आप भी सुबह-शाम देश-प्रेम किया कीजिए।’
ऐसे ही रोज के टेढ़े-मेढ़े सवालों को हल करने के लिहाज से ‘टेढ़ी बात’ की रचना हुई है, जिसमें ‘कल्पना’ का स्थान केवल उतना ही है जितना ‘सत्य’ को ‘साहित्य’ बनाने के लिए आवश्यक है। प्रत्येक रचना में लेखक की शोधी प्रवृत्ति तथा यथाशक्ति-यथासंभव ऐक्यूरेट होने की ललक समस्या या स्थिति की अनेकानेक परतें खोलने में साधक रही है।
साहित्य भाषा की कला है और भाषा की कला में डॉ. महरोत्रा खूब माहिर हैं—न कहीं एक कॉमा अधिक और न कहीं एक फुलस्टॉप कम। भाषा के यथेष्ट प्रयोग के लिए शब्दों की आत्मा में प्रवेश करके उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, वह यदि एक ओर साहित्यानुरागियों को रसाप्लावित करता चलता है तो दूसरी ओर भाषा-प्रेमियों को व्याकरण एवं प्रयोग के दृष्टांत बताता चलता है। डॉ. महरोत्रा की सुदीर्घकालीन हिंदी-सेवा से भाषा-अधिगम के लिए पुष्कल सामग्री पदे-पदे मिलती है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कुछ ऐसे स्पेलिंग और लिपि-चिह्न विकसित किए हैं, जो हिंदी की प्रकृति के लिए इष्ट और तर्कसम्मत होने के कारण विविध हिंदी-सेवियों, संस्थाओं और प्रेसों आदि को भी मान्य हैं।
कुल मिलाकर डॉ. महरोत्रा की ‘टेढ़ी बात’ कहीं दीयों के तले अँधेरे को उजागर करती है तो कहीं जन-मानस को अपने कर्तव्यों और दायित्वों का बोध कराती चलती है; कहीं वह गलतफहमी के शिकार लोगों को असलियत से वाकिफ कराती चलती है तो कहीं गलत लोगों को सही राह पर चलना सिखाती चलती है। वह एक ऐसा आइना है, जिसमें हमारे समाज की सच्ची तसवीर दिखाई देती है, जिसे देखकर एक सच्चे मानव में करुणा उपजती है। यह करुणा ही वस्तुतः लेखनी की छटपटाहट बनकर ‘टेढ़ी बात’ के रूप में ढल गई है।
साहित्य में ‘बासी’ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, साहित्य का ‘सत्य’ और अधिक मूल्यवान और प्रासंगिक होने लगता है। गनीमत है, यहाँ पुराने मॉडल का स्थान नए मॉडल नहीं ले पाते, अन्यथा कालीदास या शेक्सपीयर का नाम भी नहीं रह पाता।
हाँ, रुचि बदलती है मनुष्य की, जिससे वह पुराने में कुछ जोड़ता और उससे कुछ घटाता चलता है। ‘टेढ़ी बात’ को ‘आड़ी-टेढ़ी बात’ बनकर आने में कुछ-न-कुछ परिवर्तन-परिवर्धन तो स्वीकारना ही पड़ा है—मात्रा में भी और आस्वाद में भी। केवल शीर्षक बदल देना समाज के साथ न्याय कदापि नहीं है।
‘टेढ़ी बात’ के ‘आड़ी-टेढ़ी बात’ रूपांतरण में ‘आड़ी-टेढ़ी’ विश्लेषण गतिसूचक है—रचना की दृष्टि से और अर्थ ग्रहण की दृष्टि से, अर्थात् जब जैसी स्थिति हो, वैसा ही आड़ा-टेढ़ापन आवश्यक है। इन रचनाओं में केवल रोग नहीं, उनका उपचार भी है—कहीं सीधे ढंग से तो कहीं आड़े-टेढ़े ढंग से। देश के हित में केवल उपदेश काम नहीं आते, अतः डॉ. महरोत्रा ने कहीं-कहीं संदेश और निर्देश भी दिए हैं। साधी-सादी बातों में (हो सकता है) व्यंग्य की धार न मिले, परंतु उनसे अभीष्ट-सिद्धि में अद्भुत सहायता मिलती है—स्पष्टवादिता के कारण कंट्रास्ट के रूप में। वैसे भी किसी संकलन की सभी रचनाएँ एक ही तेवर की शायद ही होती हों। हिमालय की सारी चोटियाँ भी एवरेस्ट कहाँ हुआ करती हैं, तथापि पूरी श्रेणी हिमालय ही कहलाती है।
लेखकीय
व्यंग्य की नब्ज
मैंने एक गंभीर व्यंग्यकार से पूछा कि
‘जब
‘व्यंग’ बराबर ‘विगतं वा अंङ्गं
यस्य’ है।
(विशेषण के रूप में ‘अंगहीन, विकलांग, लुंज’ और
संज्ञा के रूप
में ‘मेढक’ भी) तो आप ‘व्यंग्य’
को कहीं
‘व्यंग्य’ और कहीं ‘व्यंग’ क्यों
लिखते हैं
?’’ वे बोले, ‘मैं स्वयं के लिखे हुए
‘व्यंग्य’ को ‘व्यंग्य’ लिखता
हूँ और दूसरों के
लिखे हुए ‘तथाकथित’ को ‘व्यंग’
लिखता हूँ !’
‘व्यंग्य’ में ‘वि’ उपसर्ग के बाद ‘व्यक्त करना, प्रकट करना, प्रस्तुत करना, स्पष्ट करना, सफाई करना, लिपाई करना’ आदि अर्थोंवाली ‘अंज्’ धातु है। इसी धातु से ‘व्यंजन, व्यंजना, व्यंजक, व्यंजित और ‘व्यक्त, व्यक्ति, अभिव्यक्त, अभिव्यक्ति’ आदि बने हैं।
‘व्यंग्य’ विशेषण के रूप में ‘व्यंजनावृत्ति द्वारा ध्वनित, परोक्ष संकेत द्वारा सूचित’ है और संज्ञा के रूप में ‘ध्वनित या उपलक्षित अर्थ’ है, जो ‘वाच्यार्थ या मुख्यार्थ और ‘लक्ष्यार्थ या गौणार्थ’ के विपरीत होता है।
‘व्यंग्य’ में ‘वि’ उपसर्ग के बाद ‘व्यक्त करना, प्रकट करना, प्रस्तुत करना, स्पष्ट करना, सफाई करना, लिपाई करना’ आदि अर्थोंवाली ‘अंज्’ धातु है। इसी धातु से ‘व्यंजन, व्यंजना, व्यंजक, व्यंजित और ‘व्यक्त, व्यक्ति, अभिव्यक्त, अभिव्यक्ति’ आदि बने हैं।
‘व्यंग्य’ विशेषण के रूप में ‘व्यंजनावृत्ति द्वारा ध्वनित, परोक्ष संकेत द्वारा सूचित’ है और संज्ञा के रूप में ‘ध्वनित या उपलक्षित अर्थ’ है, जो ‘वाच्यार्थ या मुख्यार्थ और ‘लक्ष्यार्थ या गौणार्थ’ के विपरीत होता है।
व्यंग्य की भाषा
व्यंग्य में प्रयुक्त होनेवाले शब्दों के लिए
कोई अलग
वर्णमाला या वर्तनी नहीं होती। शब्दों की धातुएँ, उपसर्ग और प्रत्यय भी
वही होते हैं, जो किसी भी प्रकार के अन्य गद्य या पद्य में होते हैं। इसी
प्रकार व्यंग्य से युक्त वाक्यों पर भी कोई नए और भिन्न व्याकरणिक नियम
लागू नहीं होते। लेकिन उसमें ‘कुछ’ जरूरत होता है, जो
‘शब्दकोश’ और ‘व्याकरण’ के
माध्यम से पकड़ में
नहीं आता। यह ‘कुछ’ शब्द-चयन और संकेतिक गूढ़ार्थ का
संबंध
होता है। उदाहरण देखें—
हरिशंकर परसाई लिखते हैं-‘चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। अब मातमपुर्सी का काम रह गया है।’ यहाँ मातमपुर्सी का प्रयोग चुनाव-परिणाम संबंधी सारे घटना-क्रम को पिक्चराइज करते हुए हारे हुए कैंडिडेट की मनोदशा और दुर्गति को व्यंजित कर रहा है।
व्यंग्य की भाषा में हमें नए-नए उपमानों का नजारा देखने को मिलता है। शंकर पुणतांबेकर के नेता द्वारा जनता को रोने से पहले ही चुप कर सुला देने के लिए ‘देशभक्ति के पालने’, ‘वायदों की डोरी’ और ‘राष्ट्रगीत की लोरी’ का सहारा लिया है।
श्रीलाल शुक्ल की एक अभिव्यक्ति है-‘गाड़ी से एक चपरासीनुमा अफसर और अफसरनुमा चपरासी उतरे।’ इसमें ‘चपरासीनुमा’ और अफसरनुमा’ विशेषणों का चयन और प्रयोग क्रमशः ‘अफसर’ और ‘चपरासी’ की क्या खूब रगड़ाई कर रहा है !
हरिशंकर परसाई लिखते हैं-‘चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। अब मातमपुर्सी का काम रह गया है।’ यहाँ मातमपुर्सी का प्रयोग चुनाव-परिणाम संबंधी सारे घटना-क्रम को पिक्चराइज करते हुए हारे हुए कैंडिडेट की मनोदशा और दुर्गति को व्यंजित कर रहा है।
व्यंग्य की भाषा में हमें नए-नए उपमानों का नजारा देखने को मिलता है। शंकर पुणतांबेकर के नेता द्वारा जनता को रोने से पहले ही चुप कर सुला देने के लिए ‘देशभक्ति के पालने’, ‘वायदों की डोरी’ और ‘राष्ट्रगीत की लोरी’ का सहारा लिया है।
श्रीलाल शुक्ल की एक अभिव्यक्ति है-‘गाड़ी से एक चपरासीनुमा अफसर और अफसरनुमा चपरासी उतरे।’ इसमें ‘चपरासीनुमा’ और अफसरनुमा’ विशेषणों का चयन और प्रयोग क्रमशः ‘अफसर’ और ‘चपरासी’ की क्या खूब रगड़ाई कर रहा है !
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book