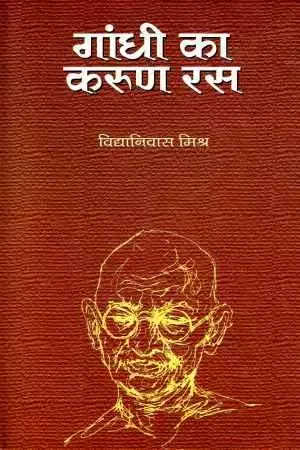|
लेख-निबंध >> गांधी का करुण रस गांधी का करुण रसविद्यानिवास मिश्र
|
326 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है गाँधी जी पर आधारित निबन्ध...
Ghandika Karuna Ras
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
गांधी जी ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी और भारत के स्वाधीन हो जाने पर उन्हें विषाद ने घेरा कि मैं इस स्वतन्त्र भारत की कुछ दिशा निर्देश नहीं दे सकता मैं अप्रासंगिक हो गया हूँ। क्या अपने जीवन की एक निरंतर मंथन बनानेवाला गांधी जैसा आदमी आप्रसंगिक हो सकता है? केवल भारत के लिए नहीं विश्वमात्र के लिए? और पशुबल के आगे हार न माननेवाला एक व्यक्ति स्वजनों से ऐसे हार मानने के लिए ऐसे विवश होगा?
मुझे तो ऐसा लगता है कि हरिलाल गांधी का जीवन हरिलाल की त्रासदी नहीं गांधी जी की त्रासदी है-और शायद यह भारत की ही त्रासदी है। भारत जीतकर हारता रहा है हारकर जीतता रहा है। इसकी संस्कृत की बुनावट में कहीं गहरी करूणा के बाज हैं। भारत की अद्भुद क्षमता है त्याग की- और इसी मात्रा में उसके लोभ की प्रबलता भी है। यह लोभ कभी-कभी धर्म का लोभ होता है, प्रतिष्ठा का लोभ होता हमें हमेशा मारता है-चाहे जौहर के रूप में मारता रहा हो या पंचशील के उपदेष्टा के रूप में। ऐसी जटिल संरचनावाले भारत के विकास के बारे में कोई भी कल्पना करें उसमें गांधी को अलग नहीं कर सकते, युधिष्ठिर को अलग नहीं कर सकते, राम और कृष्ण को अलग नहीं कर सकते, नवजात बच्चे के साथ सोई हुई यशोधरा को त्यागने वाले महानिष्क्रमण के लिए प्रस्थित बुद्ध को अलग नहीं कर सकते, तितिक्षा का पाठ पढ़ानेवाले उन महावीर के चिंतन को अलग नहीं कर सकते जो सबसे अधिक धन और धन के भोग को आकृष्ट करता है।
मुझे तो ऐसा लगता है कि हरिलाल गांधी का जीवन हरिलाल की त्रासदी नहीं गांधी जी की त्रासदी है-और शायद यह भारत की ही त्रासदी है। भारत जीतकर हारता रहा है हारकर जीतता रहा है। इसकी संस्कृत की बुनावट में कहीं गहरी करूणा के बाज हैं। भारत की अद्भुद क्षमता है त्याग की- और इसी मात्रा में उसके लोभ की प्रबलता भी है। यह लोभ कभी-कभी धर्म का लोभ होता है, प्रतिष्ठा का लोभ होता हमें हमेशा मारता है-चाहे जौहर के रूप में मारता रहा हो या पंचशील के उपदेष्टा के रूप में। ऐसी जटिल संरचनावाले भारत के विकास के बारे में कोई भी कल्पना करें उसमें गांधी को अलग नहीं कर सकते, युधिष्ठिर को अलग नहीं कर सकते, राम और कृष्ण को अलग नहीं कर सकते, नवजात बच्चे के साथ सोई हुई यशोधरा को त्यागने वाले महानिष्क्रमण के लिए प्रस्थित बुद्ध को अलग नहीं कर सकते, तितिक्षा का पाठ पढ़ानेवाले उन महावीर के चिंतन को अलग नहीं कर सकते जो सबसे अधिक धन और धन के भोग को आकृष्ट करता है।
भूमिका
इधर गांधी की पीड़ा के विषय बहुत मथते रहे। शिक्षा के प्रश्न पर, संयत जीवन के प्रश्न पर, स्वावलंबन की आवश्यकता के प्रश्न पर और जीवन को धारण करनेवाले विशाल धर्म के प्रश्न पर। गांधीजी ने आज के जीवन-मरण के प्रश्नों पर शताब्दी पूर्व लगभग सोचा, पर वे अनसुने रह गए। गांधीजी को इसका बड़ा मलाल था, मैं दो व्यक्तियों को नहीं समझ पाया-जिन्ना को और अपने बड़े छोटे हरिलाल को। दोनों महत्वाकांक्षा की बलिवेदी पर चढ़ गए और अपने जीवन की सही दिशा से ठीक उलटे मुड़ गए। दोनों गांधी के पथ के अनुगामी थे, दोनों प्रतिगामी हो गए। पर हरिलाल के जीवन के बहाव का गांधी पर बहुत गहरा असर पड़ा।
मैं उस युगद्रष्टा के विषाद को आज के आलोक में समझना चाहता हूँ। मुझसे कभी श्री रामचंद्र गांधी ने कहा था (मैंने उनसे कहा-गांधी का आना युधिष्ठिर की वापसी है। इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा था) गांधीजी अर्जुन की वापसी हैं। अजुर्न की तरह बराबर प्रश्न छेड़नेवाले, अपने भीतर और बाहर व्याप्त विराट् देवता से उत्तर माँगनेवाले, जीवन को प्रयोगशाला बनाने के लिए सदैव तैयार। आज के धुंध भरे वातावरण में इन प्रश्नों से टकराना बड़े जोखिम का काम है। लोग ऐसे प्रश्नों से कतराना चाहते हैं, जीवन की सुविधाओं के छूटने से डरते हैं, क्योंकि बड़े प्रश्न से टकराने के लिए सुविधाएँ अपने आप खिसकने लगती हैं। मैं यह जोखिम उन लोगों की ओर से उठा रहा हूँ, जो स्वाधीनता के प्रसाद का चूरा भी नहीं पा सके और चरणामृत भी उन तक पहुँचते पहुँचते टोंटी का जल हो गया। वे लोग साक्षार हुए तो अधूरे, सफल भी हुए तो कई तरह से विपन्न। उनकी ठीक पद्धति किस आधार पर सहस्राब्दियों तक टिकी रही, वे आधार आज भी हैं, कुछ उघाड़ हो जाने के कारण कमजोर जरूर हो गए हैं। उन आधारों की बात गांधी के व्याज से न की जाये तो किस व्याज से।
मेरे इन विचारों में से कुछ श्रृंखलाबद्ध रूप में साल-डेढ़ साल से ‘साहित्य अमृत’ में छपते रहे हैं। ये लोगों को रुलाने के लिए नहीं, लोगों को खिझाने के लिए भी नहीं और रिझाने के लिए या मंचीय, प्रस्तुति के लिए नहीं, बस इसलिए कि कैसी भी उतावली हो, कहीं रुककर कहाँ चले जा रहे हैं, इसपर विचार कर लेना आज बहुत आवश्यक हो गया है। यह आराम नहीं है, यह सावधानी का विराम है। एक घड़ी हमारे साथ भी हो लें। बस इतना ही।
दिल्ली
पौष, 5/2059 वि.
मैं उस युगद्रष्टा के विषाद को आज के आलोक में समझना चाहता हूँ। मुझसे कभी श्री रामचंद्र गांधी ने कहा था (मैंने उनसे कहा-गांधी का आना युधिष्ठिर की वापसी है। इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा था) गांधीजी अर्जुन की वापसी हैं। अजुर्न की तरह बराबर प्रश्न छेड़नेवाले, अपने भीतर और बाहर व्याप्त विराट् देवता से उत्तर माँगनेवाले, जीवन को प्रयोगशाला बनाने के लिए सदैव तैयार। आज के धुंध भरे वातावरण में इन प्रश्नों से टकराना बड़े जोखिम का काम है। लोग ऐसे प्रश्नों से कतराना चाहते हैं, जीवन की सुविधाओं के छूटने से डरते हैं, क्योंकि बड़े प्रश्न से टकराने के लिए सुविधाएँ अपने आप खिसकने लगती हैं। मैं यह जोखिम उन लोगों की ओर से उठा रहा हूँ, जो स्वाधीनता के प्रसाद का चूरा भी नहीं पा सके और चरणामृत भी उन तक पहुँचते पहुँचते टोंटी का जल हो गया। वे लोग साक्षार हुए तो अधूरे, सफल भी हुए तो कई तरह से विपन्न। उनकी ठीक पद्धति किस आधार पर सहस्राब्दियों तक टिकी रही, वे आधार आज भी हैं, कुछ उघाड़ हो जाने के कारण कमजोर जरूर हो गए हैं। उन आधारों की बात गांधी के व्याज से न की जाये तो किस व्याज से।
मेरे इन विचारों में से कुछ श्रृंखलाबद्ध रूप में साल-डेढ़ साल से ‘साहित्य अमृत’ में छपते रहे हैं। ये लोगों को रुलाने के लिए नहीं, लोगों को खिझाने के लिए भी नहीं और रिझाने के लिए या मंचीय, प्रस्तुति के लिए नहीं, बस इसलिए कि कैसी भी उतावली हो, कहीं रुककर कहाँ चले जा रहे हैं, इसपर विचार कर लेना आज बहुत आवश्यक हो गया है। यह आराम नहीं है, यह सावधानी का विराम है। एक घड़ी हमारे साथ भी हो लें। बस इतना ही।
दिल्ली
पौष, 5/2059 वि.
-विद्यानिवास मिश्रा
गांधी का करुण रस
2 अक्टूबर को गांधी का जन्मदिन सरकारी छुट्टी का दिन है और उनकी समाधि पर पुष्पमाला चढ़ाने का दिन है। यह समाधि बाहर से आए सम्मानित राज्य अतिथियों का पड़ाव भी है। वे हिंदुस्तान आएँगे तो उनके कार्यक्रम में यहाँ बड़ी सी माला भेंट करना अनिवार्य कर्मकांड है। गांधी का चित्र नोट पर छपता है और हर शहर में उनके नाम से एक सड़क है। दो आश्रम भी उनके नाम के हैं-एक वर्धा में, एक साबरमती के किनारे अहमदाबाद में। उनके नाम से जहाँ तक मुझे ज्ञात है, तीन-तीन विश्वविद्यालय हैं। और जहाँ तक मुझे मालूम है, उन्होंने आजाद हिंदुस्तान की व्यवस्था की जो रूपरेखा की और उसे स्वाधीनता-प्राप्ति के कई दशक पहले प्रकाशित किया, न केवल उसकी चर्चा नहीं हुई, वह कहीं पाठ्यक्रम में भी नहीं है। वैसे गांधी अध्ययन केंद्र है, शायद हर विश्वविद्यालय में होगा; पर गांधीजी के चिंतन में जो नक्शा हिंदुस्तान का बना वह कहीं ताक पर रख दिया गया है। इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी ! जिस समय देश का विभाजन हो गया और एकता का स्वप्न टूटने से नैराश्य के बावजूद गांधीजी सपने सँजो रहे थे कि किसी दिन यह अस्वाभाविक विभाजन जुड़ाव में परिवर्तित होगा और इसीलिए वे लोकप्रियता को दाँव पर चढ़ाकर हमारी जो देनदारी पाकिस्तान पर थी उसे चुकता मनवाने पर अड़ गए, जिस पर बड़ा आक्रोश हुआ। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में वे बिलकुल अकेले पड़ गए थे। उन्होंने एकाधिक बार प्रार्थना सभा में कहा, ‘लोग मुझे पागल समझते हैं। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ।’ गांधीजी ऐसे अकेले नहीं थे। उनके पास दुर्दम्य आस्तिकता का संबल था और यह आस्तिकता भी स्वतंत्र भारत में करुणांत ही सिद्ध हुई। गांधीजी का समग्र विचार गांधीजी के साथ ही विदा हो गया। उनपर अमल करने का जिन्होंने व्रत लिया उन्होंने अतिरेक से काम लिया और गांधीवादी आंदोलन असहाय, निरुपाय आंदोलन में परिणत हुआ।
इसकी एक दुरंत कथा है। स्वतंत्र भारत ने स्वतंत्रता को स्वावलंबन से किस दिन से अलग किया, यह खोज का विषय है; पर परावलंब ही स्वाघीनता की रक्षा का उपाय हो गया तथा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक रूपी स्तरों पर हिंदुस्तान आयात पर अवलंबित होता गया। निर्यात के नाम पर उसके पास नृत्य रह गया और साल में भेजे जानेवाले सद्भावना मंडल रह गए। गांधीजी नामशेष रह गए। उनके विचार यदि रहे भी तो निराकार में रहे। इस त्रासदी पर रचनात्मक चिंतन भी बहुत कम हुआ। जहाँ तक मुझे स्मरण है, उनकी मृत्यु पर सबसे सार्थक शोक-गीत स्वर्गीय बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’ ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने गांधी की मृत्यु पर शोक नहीं, गांधी की हत्या करने की स्थिति, हत्या जिस कारण हुई उस कारण पर-मानवता की मृत्यु पर उन्होंने शोक व्यक्त किया। यह मानवता क्या थी, इसके निहितार्थ क्या थे-इसपर एक पीढ़ी, गुजरी, दो पीढ़ियाँ, गुजरीं, तीसरी पीढ़ी सामने आ गई-कोई जुंबिश नहीं हुई। अभी-अभी मुझे दिनकर जोशी की पुस्तक का हिंदी अनुवाद ‘उजाले की परछाईं’ पढ़ने को मिला। वैसे तो यह जीवन-कथा गांधीजी के बड़े पुत्र हरिलाल गांधी की है, जो गांधीजी के अत्यंत प्रिय बड़े बेटे होकर और उनके दक्षिण अफ्रीका के अभियान को आगे बढ़ाने के कारण छोटे गांधी होकर भी एक दिन बगावत पर उतर आए और एक भंयकर आकर्षण-विकर्षण के शिकार हुए। वे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कोशिश करने लगे और लड़खड़ाते ही चले गए। पर गांधीजी के आदर्श उनके सिर पर सवार रहे। वे परिवारी बनना चाहते थे, परिवार-विहीन होकर बेनाम मरे। गांधीजी के जाने के लगभग चार-पाँच महीने बाद। उनके लिए उनकी माँ जीवन भर बिलखती रहीं। गांधीजी के मन में भी अंतर्द्वंद्व रहा कि मुझसे क्या गलती हुई। उन्होंने तो अपने को एक बड़े परिवार का कर्ता माना, इसलिए अपने बड़े बेटे की उत्कट इच्छा होते हुए भी, किसी दूसरे का मुक्त निमंत्रण होते हुए भी कि आपके किसी एक लड़के को लंदन में पढ़ाना चाहता हूँ-उन्होंने पहले तो एक भतीजे को भेजा, जो बीच में ही लौट आया, फिर एक पारसी सज्जन को भेजा। गांधीजी सोचते थे कि जो कठिन तप की शिक्षा उनके आश्रम में दी गई है, उससे बड़ी शिक्षा कोई नहीं है। हरिलाल गांधी अपनी कल्पना की शिक्षा के लिए तरसते ही रह गए। वे यह शिक्षा अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए पाना चाहते थे। परिवार को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाने के लिए प्राप्त करना चाहते थे। गांधीजी के मन में अवश्य अंतर्द्वंद्व रहा होगा और हरिलाल गांधी के लिए करुणा भी रही होगी। उन्होंने हरिलाल गांधी को दक्षिण अफ्रीका से विदा देते समय संबोधित करके कहा भी था-मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना।
ऐसा ही अंतर्द्वंद्व राम के मन में भी हुआ होगा, जब उन्होंने लोकापवाद की अधिक चिंता की और सीता को निर्वासित किया। हरिलाल गांधी सीता तो नहीं थे; पर जीवन में इतने अतिचारों के बावजूद वे अनगढ़ आजाद हीरा तो थे ही। नहीं तो माँ और पिता दोनों के अंतिम दर्शन करने वे दूर-दराज से खिंचे न आते। उनसे जो भी गलतियाँ हुईं उन गलतियों पर आज विचार होना आवश्यक है। गांधीजी हिंदुस्तान के आम आदमी के ही दुःख से नहीं, किसी भी पराधीन प्राणी के दुःख से द्रवित हो जाते थे। उनकी मानवता समस्त जड़-चेतन को समेटकर क्रियाशील होती थी; पर वे अपने पुत्र के प्रति इतने अकरुण क्यों हुए ? यह सोचना कि उन्हें अपनी छवि की चिंता थी, सरासर अन्याय होगा। गांधीजी अपना सर्वस्व उत्सर्ग करनेवाली बा के प्रति भी कई बार अकरुण हुए। पर बा के लिए उनके मन में अगाध प्यार था। बा के जाने के बाद गांधीजी की ऊर्जा आधी से अधिक चली गई, नहीं तो गांधीजी ने विभाजन होने नहीं दिया होता, अकेले उनमें इतना दम था। गांधीजी को अपनी छवि की चिंता नहीं थी, ऐसे देश की छवि की चिंता थी जो देश के बाहर के बारे में भी सोचने का अभ्यासी रहा। जो गांधी बकरी को परिवार का अंग बना सकते थे वे गांधी अपने लड़के के बारे में यह उद्घोषणा करें कि यह मेरा लड़का नहीं रहा, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, बड़ा ही अकरुण निर्णय है।
यहीं पर गांधीजी का जीवन उस सनातन प्रश्न को छेड़ता है कि कितनी दूर तक लोक की चिंता और कितनी दूर तक अपने निजी संबंधों की चिंता। क्या इन दोनों में विरोध है ? यदि है तो क्या उसका समाधान नहीं है ? यह प्रश्न आज भी किसी भी संवेदनशील आदमी को उतना ही सालेगा जितना गांधीजी को सालता रहा होगा। एक प्रश्न और है। जिस स्वदेशी का दर्शन गांधीजी ने दिया वह स्वदेशी देश के सौष्ठव से कितना जुड़ी। गांधीजी ने तो मन, हाथ और आँख तीनों के सहयोग को ही शिक्षा का प्रथम सोपान कहा। पर उन्होंने शायद चित्र को छोड़ दिया। नहीं तो महादेव देसाई गिरिसप्पा जलप्रपात देखना चाहते थे, उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली-तब रवींद्र केडेकर ने गांधीजी के संबंध में एक लंबी चर्चा काका कालेलकर से की। वहा चर्चा गांधीजी के अंतर्विरोधों को समझने में आज भी बड़ी उपयोगी है। आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक ‘आर्ट और स्वदेशी’ में बहुत सारे मर्मभेदी प्रश्न छेड़े। मैंने पृथ्वी सिंह आजाद से, जो गांधीजी के आश्रय में कुछ दिनों आश्रय लिये हुए थे बहुत सी कथाएँ सुनी थीं। उनसे मुझे लगा था कि विग्रह का अतिरेक कभी-कभी आसक्ति को उकसाता है। ऐसा क्यों होता है ? गांधीजी ने ‘गीता’ पढ़ी ही नहीं थी, गुनी भी थी और श्रीकृष्ण के निष्काम योग के वे साधक भी थे। पर उन्होंने कर्म के कौशल में तो सौंदर्य देखा, सौंदर्य में नियंता का कौशल क्यों नहीं देखा ?
जिस प्रकार के आर्थिक-सामाजिक ढाँचे की उन्होंने कल्पना की उसमें उत्सव का उल्लास क्यों नहीं रहा ? मैंने उसके दोनों आश्रयों को उनके जाने के बाद देखा। हृदयकुंज को भी, सेवागुरु को भी। दोनों जड़, दोनों में ऐसा तो लगता है कि गांधीजी कहीं उपस्थित हैं, पर बिहँसते हुए गांधी नहीं, थके-हारे गांधी वहाँ उपस्थित हैं। सबसे अलग, बिछुड़े हुए धीरे-धीरे पहाड़ की ओर चढ़ते हुए युधिष्ठिर की तरह गांधीजी चल रहे हैं-सब छूटते जा रहे हैं, कोई भी सगा आदमी साथ नहीं दे पाता। युधिष्ठिर ने धर्म की लड़ाई लड़ी, अन्याय न सहने की लड़ाई लड़ी, पर लड़ाई जीत जाने पर उन्हें विषाद ने घेरा। गांधीजी ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी और भारत के स्वाधीन हो जाने पर उन्हें विषाद ने घेरा कि मैं इस स्वतंत्र भारत में कुछ दिशा-निर्देश नहीं दे सकता। मैं अप्रासंगिक हो गया हूँ। क्या अपने जीवन को एक निरन्तर मंथन बनाने वाला गांधी जैसा आदमी अप्रासंगिक हो सकता है ? केवल भारत के लिए नहीं, विश्वमात्र के लिए ? और पशु बल के आगे हार न माननेवाला एक व्यक्ति स्वजनों से ऐसे हार मानने के लिए विवश होगा ? मुझे तो ऐसा लगता है कि हरिलाल गांधी का जीवन हरिलाल की त्रासदी नहीं, गांधीजी की भी त्रासदी है और शायद यह भारत की ही त्रासदी है। भारत जीतकर हारता रहा है और हारकर जीतता रहा है। इसकी संस्कृति की बुनावट में कहीं गहरी करुणा के बीज हैं। भारत में अद्भुत क्षमता है त्याग की, और उसी मात्रा में उससे लोभ की प्रबलता भी है। यह लोभ कभी-कभी धर्म का लोभ होता है प्रतिष्ठा का लोभ होता है, यह सकारात्मक लोभ हमें हमेशा मारता रहता है। चाहे जौहर के रूप में मारता रहा हो, चाहे पंचशील के उपदेष्टा के रूप में। ऐसे जटिल संरचना वाले भारत के विकास के बारे में कोई भी कल्पना करें, उसमें गांधी को अलग नहीं कर सकते, युधिष्ठिर को अलग नहीं कर सकते, राम और कृष्ण को अलग नहीं कर सकते, नवजात बच्चे के साथ सोई हुई यशोधरा को तजनेवाले महानिष्क्रमण के लिए प्रस्थित बुद्ध को अलग नहीं कर सकते, तितिक्षा का पाठ पढ़ानेवाले उन महावीर के चिंतन को अलग नहीं कर सकते, जो सबसे अधिक धन और धन के भोग को आकृष्ट करता है। हिंदी में गिरिराज किशोर ने गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए अभियान का लेखा-जोखा ‘पहला गिरमिटिया’ के रूप में प्रस्तुत किया है। पर दक्षिण अफ्रीका तो गांधीजी की प्राथमिक शाला था। उसके बाद उनके सारे प्रयोग भारत में हुए। उन्होंने कोयले को ही अपनी ऊर्जा के ताप से हीरा बनाया और उनका अपना हीरा कोयला बन गया। हमारे देश में या तो उन्हें महिमा के आलोक में छिपा रखा है या फिर उनको प्रतिगामी, सर्वहारा का शत्रु, पूँजीवाद का हथियार आदि एक-से-एक लफ्फाजी भरे विशेषणों से घेर रखा है। गांधीजी दोनों नहीं थे, वे नर के भीतर नारायण की बेसँभाल व्यथा थे।
काश कि वह व्यथा आज देश के हृदय पर अंकित होती तो देश के चित्त का ऐसा संस्कार होता कि सारी खामियों के बावजूद हम सही माने में स्वाधीन होने के लिए खड़े हो जाते। मन में इतना विश्वास अवश्य है कि एक-न-एक दिन गांधी की वह विराट् व्यथा उसी तरह हमारे हृदय में करुणा की रसधार बनेगी, जिस तरह ‘महाभारत’ में युधिष्ठिर का विषाद बना, श्रीकृ़ष्ण का अकेलापन बना; राजा राम की सीता के बिना जीवन की व्यर्थता का दुःख बना। तभी देश का चित्त पखारा जाएगा और शुद्ध चित्त से देश के विकास की चिंता होगी।
इसकी एक दुरंत कथा है। स्वतंत्र भारत ने स्वतंत्रता को स्वावलंबन से किस दिन से अलग किया, यह खोज का विषय है; पर परावलंब ही स्वाघीनता की रक्षा का उपाय हो गया तथा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक रूपी स्तरों पर हिंदुस्तान आयात पर अवलंबित होता गया। निर्यात के नाम पर उसके पास नृत्य रह गया और साल में भेजे जानेवाले सद्भावना मंडल रह गए। गांधीजी नामशेष रह गए। उनके विचार यदि रहे भी तो निराकार में रहे। इस त्रासदी पर रचनात्मक चिंतन भी बहुत कम हुआ। जहाँ तक मुझे स्मरण है, उनकी मृत्यु पर सबसे सार्थक शोक-गीत स्वर्गीय बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’ ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने गांधी की मृत्यु पर शोक नहीं, गांधी की हत्या करने की स्थिति, हत्या जिस कारण हुई उस कारण पर-मानवता की मृत्यु पर उन्होंने शोक व्यक्त किया। यह मानवता क्या थी, इसके निहितार्थ क्या थे-इसपर एक पीढ़ी, गुजरी, दो पीढ़ियाँ, गुजरीं, तीसरी पीढ़ी सामने आ गई-कोई जुंबिश नहीं हुई। अभी-अभी मुझे दिनकर जोशी की पुस्तक का हिंदी अनुवाद ‘उजाले की परछाईं’ पढ़ने को मिला। वैसे तो यह जीवन-कथा गांधीजी के बड़े पुत्र हरिलाल गांधी की है, जो गांधीजी के अत्यंत प्रिय बड़े बेटे होकर और उनके दक्षिण अफ्रीका के अभियान को आगे बढ़ाने के कारण छोटे गांधी होकर भी एक दिन बगावत पर उतर आए और एक भंयकर आकर्षण-विकर्षण के शिकार हुए। वे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कोशिश करने लगे और लड़खड़ाते ही चले गए। पर गांधीजी के आदर्श उनके सिर पर सवार रहे। वे परिवारी बनना चाहते थे, परिवार-विहीन होकर बेनाम मरे। गांधीजी के जाने के लगभग चार-पाँच महीने बाद। उनके लिए उनकी माँ जीवन भर बिलखती रहीं। गांधीजी के मन में भी अंतर्द्वंद्व रहा कि मुझसे क्या गलती हुई। उन्होंने तो अपने को एक बड़े परिवार का कर्ता माना, इसलिए अपने बड़े बेटे की उत्कट इच्छा होते हुए भी, किसी दूसरे का मुक्त निमंत्रण होते हुए भी कि आपके किसी एक लड़के को लंदन में पढ़ाना चाहता हूँ-उन्होंने पहले तो एक भतीजे को भेजा, जो बीच में ही लौट आया, फिर एक पारसी सज्जन को भेजा। गांधीजी सोचते थे कि जो कठिन तप की शिक्षा उनके आश्रम में दी गई है, उससे बड़ी शिक्षा कोई नहीं है। हरिलाल गांधी अपनी कल्पना की शिक्षा के लिए तरसते ही रह गए। वे यह शिक्षा अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए पाना चाहते थे। परिवार को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाने के लिए प्राप्त करना चाहते थे। गांधीजी के मन में अवश्य अंतर्द्वंद्व रहा होगा और हरिलाल गांधी के लिए करुणा भी रही होगी। उन्होंने हरिलाल गांधी को दक्षिण अफ्रीका से विदा देते समय संबोधित करके कहा भी था-मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना।
ऐसा ही अंतर्द्वंद्व राम के मन में भी हुआ होगा, जब उन्होंने लोकापवाद की अधिक चिंता की और सीता को निर्वासित किया। हरिलाल गांधी सीता तो नहीं थे; पर जीवन में इतने अतिचारों के बावजूद वे अनगढ़ आजाद हीरा तो थे ही। नहीं तो माँ और पिता दोनों के अंतिम दर्शन करने वे दूर-दराज से खिंचे न आते। उनसे जो भी गलतियाँ हुईं उन गलतियों पर आज विचार होना आवश्यक है। गांधीजी हिंदुस्तान के आम आदमी के ही दुःख से नहीं, किसी भी पराधीन प्राणी के दुःख से द्रवित हो जाते थे। उनकी मानवता समस्त जड़-चेतन को समेटकर क्रियाशील होती थी; पर वे अपने पुत्र के प्रति इतने अकरुण क्यों हुए ? यह सोचना कि उन्हें अपनी छवि की चिंता थी, सरासर अन्याय होगा। गांधीजी अपना सर्वस्व उत्सर्ग करनेवाली बा के प्रति भी कई बार अकरुण हुए। पर बा के लिए उनके मन में अगाध प्यार था। बा के जाने के बाद गांधीजी की ऊर्जा आधी से अधिक चली गई, नहीं तो गांधीजी ने विभाजन होने नहीं दिया होता, अकेले उनमें इतना दम था। गांधीजी को अपनी छवि की चिंता नहीं थी, ऐसे देश की छवि की चिंता थी जो देश के बाहर के बारे में भी सोचने का अभ्यासी रहा। जो गांधी बकरी को परिवार का अंग बना सकते थे वे गांधी अपने लड़के के बारे में यह उद्घोषणा करें कि यह मेरा लड़का नहीं रहा, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, बड़ा ही अकरुण निर्णय है।
यहीं पर गांधीजी का जीवन उस सनातन प्रश्न को छेड़ता है कि कितनी दूर तक लोक की चिंता और कितनी दूर तक अपने निजी संबंधों की चिंता। क्या इन दोनों में विरोध है ? यदि है तो क्या उसका समाधान नहीं है ? यह प्रश्न आज भी किसी भी संवेदनशील आदमी को उतना ही सालेगा जितना गांधीजी को सालता रहा होगा। एक प्रश्न और है। जिस स्वदेशी का दर्शन गांधीजी ने दिया वह स्वदेशी देश के सौष्ठव से कितना जुड़ी। गांधीजी ने तो मन, हाथ और आँख तीनों के सहयोग को ही शिक्षा का प्रथम सोपान कहा। पर उन्होंने शायद चित्र को छोड़ दिया। नहीं तो महादेव देसाई गिरिसप्पा जलप्रपात देखना चाहते थे, उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली-तब रवींद्र केडेकर ने गांधीजी के संबंध में एक लंबी चर्चा काका कालेलकर से की। वहा चर्चा गांधीजी के अंतर्विरोधों को समझने में आज भी बड़ी उपयोगी है। आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक ‘आर्ट और स्वदेशी’ में बहुत सारे मर्मभेदी प्रश्न छेड़े। मैंने पृथ्वी सिंह आजाद से, जो गांधीजी के आश्रय में कुछ दिनों आश्रय लिये हुए थे बहुत सी कथाएँ सुनी थीं। उनसे मुझे लगा था कि विग्रह का अतिरेक कभी-कभी आसक्ति को उकसाता है। ऐसा क्यों होता है ? गांधीजी ने ‘गीता’ पढ़ी ही नहीं थी, गुनी भी थी और श्रीकृष्ण के निष्काम योग के वे साधक भी थे। पर उन्होंने कर्म के कौशल में तो सौंदर्य देखा, सौंदर्य में नियंता का कौशल क्यों नहीं देखा ?
जिस प्रकार के आर्थिक-सामाजिक ढाँचे की उन्होंने कल्पना की उसमें उत्सव का उल्लास क्यों नहीं रहा ? मैंने उसके दोनों आश्रयों को उनके जाने के बाद देखा। हृदयकुंज को भी, सेवागुरु को भी। दोनों जड़, दोनों में ऐसा तो लगता है कि गांधीजी कहीं उपस्थित हैं, पर बिहँसते हुए गांधी नहीं, थके-हारे गांधी वहाँ उपस्थित हैं। सबसे अलग, बिछुड़े हुए धीरे-धीरे पहाड़ की ओर चढ़ते हुए युधिष्ठिर की तरह गांधीजी चल रहे हैं-सब छूटते जा रहे हैं, कोई भी सगा आदमी साथ नहीं दे पाता। युधिष्ठिर ने धर्म की लड़ाई लड़ी, अन्याय न सहने की लड़ाई लड़ी, पर लड़ाई जीत जाने पर उन्हें विषाद ने घेरा। गांधीजी ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी और भारत के स्वाधीन हो जाने पर उन्हें विषाद ने घेरा कि मैं इस स्वतंत्र भारत में कुछ दिशा-निर्देश नहीं दे सकता। मैं अप्रासंगिक हो गया हूँ। क्या अपने जीवन को एक निरन्तर मंथन बनाने वाला गांधी जैसा आदमी अप्रासंगिक हो सकता है ? केवल भारत के लिए नहीं, विश्वमात्र के लिए ? और पशु बल के आगे हार न माननेवाला एक व्यक्ति स्वजनों से ऐसे हार मानने के लिए विवश होगा ? मुझे तो ऐसा लगता है कि हरिलाल गांधी का जीवन हरिलाल की त्रासदी नहीं, गांधीजी की भी त्रासदी है और शायद यह भारत की ही त्रासदी है। भारत जीतकर हारता रहा है और हारकर जीतता रहा है। इसकी संस्कृति की बुनावट में कहीं गहरी करुणा के बीज हैं। भारत में अद्भुत क्षमता है त्याग की, और उसी मात्रा में उससे लोभ की प्रबलता भी है। यह लोभ कभी-कभी धर्म का लोभ होता है प्रतिष्ठा का लोभ होता है, यह सकारात्मक लोभ हमें हमेशा मारता रहता है। चाहे जौहर के रूप में मारता रहा हो, चाहे पंचशील के उपदेष्टा के रूप में। ऐसे जटिल संरचना वाले भारत के विकास के बारे में कोई भी कल्पना करें, उसमें गांधी को अलग नहीं कर सकते, युधिष्ठिर को अलग नहीं कर सकते, राम और कृष्ण को अलग नहीं कर सकते, नवजात बच्चे के साथ सोई हुई यशोधरा को तजनेवाले महानिष्क्रमण के लिए प्रस्थित बुद्ध को अलग नहीं कर सकते, तितिक्षा का पाठ पढ़ानेवाले उन महावीर के चिंतन को अलग नहीं कर सकते, जो सबसे अधिक धन और धन के भोग को आकृष्ट करता है। हिंदी में गिरिराज किशोर ने गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए अभियान का लेखा-जोखा ‘पहला गिरमिटिया’ के रूप में प्रस्तुत किया है। पर दक्षिण अफ्रीका तो गांधीजी की प्राथमिक शाला था। उसके बाद उनके सारे प्रयोग भारत में हुए। उन्होंने कोयले को ही अपनी ऊर्जा के ताप से हीरा बनाया और उनका अपना हीरा कोयला बन गया। हमारे देश में या तो उन्हें महिमा के आलोक में छिपा रखा है या फिर उनको प्रतिगामी, सर्वहारा का शत्रु, पूँजीवाद का हथियार आदि एक-से-एक लफ्फाजी भरे विशेषणों से घेर रखा है। गांधीजी दोनों नहीं थे, वे नर के भीतर नारायण की बेसँभाल व्यथा थे।
काश कि वह व्यथा आज देश के हृदय पर अंकित होती तो देश के चित्त का ऐसा संस्कार होता कि सारी खामियों के बावजूद हम सही माने में स्वाधीन होने के लिए खड़े हो जाते। मन में इतना विश्वास अवश्य है कि एक-न-एक दिन गांधी की वह विराट् व्यथा उसी तरह हमारे हृदय में करुणा की रसधार बनेगी, जिस तरह ‘महाभारत’ में युधिष्ठिर का विषाद बना, श्रीकृ़ष्ण का अकेलापन बना; राजा राम की सीता के बिना जीवन की व्यर्थता का दुःख बना। तभी देश का चित्त पखारा जाएगा और शुद्ध चित्त से देश के विकास की चिंता होगी।
भय, आंतक और हिंसा
मनुष्य का सहज स्वभाव भय नहीं, अभय है। ऐसा न होता तो बच्चा साँप से, आग से खेलना नहीं चाहता। शकुंतला का बेटा सर्वदमन मुँह बाए सिंह के दाँत गिनने के लिए जिद न करता। भय बच्चा समाज से अर्जित करता है। पहले वह उसे लीला भाव से लेता है और जैसे-जैसे उसे डरवाया गया है वैसे-वैसे वह डरवाने की नकल उतारता है। भय का और भी भयानक रूप यह होता है कि उसे इतिहास की स्मृति आक्रांत करती है। एक जाति दूसरी जाति से सदियों आक्रांत और पराभूत होने के बाद ऐसी स्थिति में पहुँच जाती है कि उस जाति से भयभीत अंग बन जाता है। मेरे एक विदेशी कवि मित्र हिंदुस्तान आए। एकाध महीना घूमे और कहा, ‘अद्भुत है कि यहां बहुसंख्यक अल्पसंख्यक-भय से पूरी तरह ग्रस्त हैं।’ उल्लेखनीय है कि यह भय जन्म से नहीं होता, न यह भय कभी जीवकोश में छाप छोड़ता है। इस भय में लोगों को शिक्षित किया जाता है। यही अर्जित भय धीरे-धीरे अनेक तरह की सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करने लगता है। उसके भीतर अकारण असुरक्षा का भाव जाग्रत होता है। इसी का परिणाम होता है अलग बस्ती का बसना, अलग घरौंदों, का बनना जिसमें हर घरौंदा दूसरे घरौंदे-समूह को संदेह की दृष्टि से देखने लगता है। असुरक्षा की गाँठ जब कस जाती है तो भय आतंक बन जाता है। तब दूसरे को चोट पहुँचाने में ही अपनी सुरक्षा सधती दिखती है।
भय का नियत संबंध इस मूल भावना से है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा कहते और करते हैं, वही न केवल सत्य है बल्कि वही एकमात्र सत्य है। उसे जो नहीं स्वीकार करता वह असत्य है। ऐसे व्यक्ति की जब तक स्थिति रहेगी तब तक हमारी अद्वितीयता सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए उससे या तो अपनी बात मनवाओ या उसे इस लायक न रखो कि वह अपनी बात को सच कह सके। यहीं हिंसा जन्म लेती है। हिंसा कभी भी आत्मबलवाले व्यक्ति या सहज व्यक्ति के मन में नहीं उपजती। आदमी भीतर से जितना ही कमजोर, जितना ही असहज होगा उतना ही उसके हिंस्र होने की आशंका रहती है। इस हिंसा को वैध मनवाने के लिए, इसकी अवैधता को दूर करने के लिए युद्ध होता है। इस प्रकार भय से युद्ध तक एक सहज बनी हुई श्रृंखला है।
इससे ठीक उलटे अभय की स्थिति है। सत्त्व गुण-संपन्न व्यक्ति के अनेक लक्षणों में एक लक्षण है अभय। अभय समाज के फैलाए हुए जाल से मुक्ति है। ये जाल कई प्रकार के हो सकते हैं-आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, और सबसे खतरनाक जाल वे हैं जो तथाकथित रूप में धार्मिक होते हैं। भोजपुरी में एक कहावत है, जिसका हिंदी रूपांतर होगा कि सब पापों से बचें तो आषाढ़ में सत्तू खाने से कोई पाप नहीं लगेगा, अर्थात् जिन वर्जनाओं की बात से डराया जाता है वे मुख्य नहीं हैं। मुख्य है वह सहज भाव, जिसके कारण कोई जीवन केवल विधि रूप होता है, वह कभी निषेध नहीं होता। विधि रूप जीवन भी अनायास होता है, किसी से प्रेरित होकर नहीं होता। यह अनायास होना घटित तब होता है जब मनुष्य सब में अपने को देखने-पाने लगता है और सबको अपने भीतर उदार मन से भरने लगता है। ऐसा अभ्यास हो जाय तो जो भी मनुष्य से होगा वह सर्वमय होगा, वह विधि रूप होगा, वह समस्त सृष्टि का प्रयोजन होगा। सृष्टि आखिर इसी प्रयोजन से विस्तार पाती है कि दूसरे में अपने को पाएँगे, तभी अपनी सार्थकता होगी। इसीलिए एक को दो, दो को तीन और इसी तरह अंत में अनंत होना चाहिए। यह भाव सत्त्व-संशुद्धि है। ऐसा नहीं है जैसा कि किसी ज्ञानी के भाषण में घटित हुआ। वे सभा को संबोधित करने चले तो शुरू किया-भाइयो, बहनो और माताओ !....एकाएक उनकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ी और उन्होंने संबोधन में संशोधन किया-आगे कुरसी पर बैठी हुई उस नीली सलवारवाली को छोड़कर। ऐसे सहज भाव में प्रतिष्ठित होने पर यह प्रार्थना नहीं होती कि प्रभु, जो हमारे मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हीं पर अपनी कृपा करना, दूसरों पर नहीं। हमें बल देना कि हम दूसरों पर ऐसे हावी हों कि वे हमारी रीति-नीति पूरी तरह अपना लें। इस प्रकार सहजता, अभय, सत्त्व-संशुद्धि, सर्वहित की चिंता-इन सबकी अपने आप एक लड़ी बन जाती है।
भय का नियत संबंध इस मूल भावना से है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा कहते और करते हैं, वही न केवल सत्य है बल्कि वही एकमात्र सत्य है। उसे जो नहीं स्वीकार करता वह असत्य है। ऐसे व्यक्ति की जब तक स्थिति रहेगी तब तक हमारी अद्वितीयता सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए उससे या तो अपनी बात मनवाओ या उसे इस लायक न रखो कि वह अपनी बात को सच कह सके। यहीं हिंसा जन्म लेती है। हिंसा कभी भी आत्मबलवाले व्यक्ति या सहज व्यक्ति के मन में नहीं उपजती। आदमी भीतर से जितना ही कमजोर, जितना ही असहज होगा उतना ही उसके हिंस्र होने की आशंका रहती है। इस हिंसा को वैध मनवाने के लिए, इसकी अवैधता को दूर करने के लिए युद्ध होता है। इस प्रकार भय से युद्ध तक एक सहज बनी हुई श्रृंखला है।
इससे ठीक उलटे अभय की स्थिति है। सत्त्व गुण-संपन्न व्यक्ति के अनेक लक्षणों में एक लक्षण है अभय। अभय समाज के फैलाए हुए जाल से मुक्ति है। ये जाल कई प्रकार के हो सकते हैं-आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, और सबसे खतरनाक जाल वे हैं जो तथाकथित रूप में धार्मिक होते हैं। भोजपुरी में एक कहावत है, जिसका हिंदी रूपांतर होगा कि सब पापों से बचें तो आषाढ़ में सत्तू खाने से कोई पाप नहीं लगेगा, अर्थात् जिन वर्जनाओं की बात से डराया जाता है वे मुख्य नहीं हैं। मुख्य है वह सहज भाव, जिसके कारण कोई जीवन केवल विधि रूप होता है, वह कभी निषेध नहीं होता। विधि रूप जीवन भी अनायास होता है, किसी से प्रेरित होकर नहीं होता। यह अनायास होना घटित तब होता है जब मनुष्य सब में अपने को देखने-पाने लगता है और सबको अपने भीतर उदार मन से भरने लगता है। ऐसा अभ्यास हो जाय तो जो भी मनुष्य से होगा वह सर्वमय होगा, वह विधि रूप होगा, वह समस्त सृष्टि का प्रयोजन होगा। सृष्टि आखिर इसी प्रयोजन से विस्तार पाती है कि दूसरे में अपने को पाएँगे, तभी अपनी सार्थकता होगी। इसीलिए एक को दो, दो को तीन और इसी तरह अंत में अनंत होना चाहिए। यह भाव सत्त्व-संशुद्धि है। ऐसा नहीं है जैसा कि किसी ज्ञानी के भाषण में घटित हुआ। वे सभा को संबोधित करने चले तो शुरू किया-भाइयो, बहनो और माताओ !....एकाएक उनकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ी और उन्होंने संबोधन में संशोधन किया-आगे कुरसी पर बैठी हुई उस नीली सलवारवाली को छोड़कर। ऐसे सहज भाव में प्रतिष्ठित होने पर यह प्रार्थना नहीं होती कि प्रभु, जो हमारे मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हीं पर अपनी कृपा करना, दूसरों पर नहीं। हमें बल देना कि हम दूसरों पर ऐसे हावी हों कि वे हमारी रीति-नीति पूरी तरह अपना लें। इस प्रकार सहजता, अभय, सत्त्व-संशुद्धि, सर्वहित की चिंता-इन सबकी अपने आप एक लड़ी बन जाती है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book