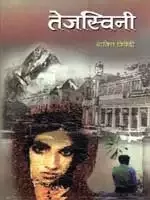|
कहानी संग्रह >> तेजस्विनी तेजस्विनीशक्ति त्रिवेदी
|
438 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है श्रेष्ठ कहानी संग्रह...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
आज इस आकस्मिक घटना से हम दोनों के हृदय में ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ी।
हमें लगा की मानों कोई दिव्य शक्ति हमारी ओर हाथ बढ़ाने वाली है। हमें
शीघ्र ही विपत्ति से छुटकारा मिलने वाला है। विपत्तियाँ स्थायी नहीं
होतीं। जब व्यक्ति सब ओर से निराश हो जाता है, तभी प्रभु उसकी सहायता करते
है।
कृष्णा का घर में सम्मान था। भाई-भतीजे आदि सभी उसे सम्मान से रखते थे; उसकी माँ तथा भाई राधामोहन उसे ? कृष्णा कहकर पुकारते थे, पर कांता जब छोटी थी, वह उसे कृष्णा दीदी न कहकर ‘निन्ना दीदी’ कहा करती थी। और तभी से सब लोग उसे निन्ना कहने लगे। कृष्णा पढ़ी लिखी तो थी ही। उसका स्वाभाव बड़ा मिलनसार और भाषा, बोली मधुर थी। उसके ओठों पर हर समय मुस्कान फैली रहती थी।
सन् 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय भी ईसाई समाज हिंदू ब्राह्मण वर्ग से पूर्ण बहिष्कृत और उपेक्षित था। गरीब ब्राह्मण सत्ताधारी प्रभु वर्ग के अंग्रेज ईसाइयों को तुच्छ समझते थे। स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहना ही उनका दंभ था। इसी समय में अंग्रेज ईसाई महिला सॉफी और शर्मा के प्रेम संबंध उस युग की एक सामाजिक क्रान्तिकारी घटना थी। वास्तव में मानव प्रेम धर्म जाति संप्रदाय और संकीर्णता पर नहीं टिका है।
लहना सिंह इलाके का हिस्ट्रीशीटर भी था; पर भगवान ने उसे गला इतना मीठा दिया था कि उसकी आवाज सुनने के लिए लोग दूर-दूर से आते थे। स्वयं थाने के लोग भी उसे बिठाकर फिल्मी गीत सुना करते थे। नामी चोर होते हुए भी लहना सिंह का अंदाज चाल ढाल किसी मस्ताने हीरो से कम न थी।
कृष्णा का घर में सम्मान था। भाई-भतीजे आदि सभी उसे सम्मान से रखते थे; उसकी माँ तथा भाई राधामोहन उसे ? कृष्णा कहकर पुकारते थे, पर कांता जब छोटी थी, वह उसे कृष्णा दीदी न कहकर ‘निन्ना दीदी’ कहा करती थी। और तभी से सब लोग उसे निन्ना कहने लगे। कृष्णा पढ़ी लिखी तो थी ही। उसका स्वाभाव बड़ा मिलनसार और भाषा, बोली मधुर थी। उसके ओठों पर हर समय मुस्कान फैली रहती थी।
सन् 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय भी ईसाई समाज हिंदू ब्राह्मण वर्ग से पूर्ण बहिष्कृत और उपेक्षित था। गरीब ब्राह्मण सत्ताधारी प्रभु वर्ग के अंग्रेज ईसाइयों को तुच्छ समझते थे। स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहना ही उनका दंभ था। इसी समय में अंग्रेज ईसाई महिला सॉफी और शर्मा के प्रेम संबंध उस युग की एक सामाजिक क्रान्तिकारी घटना थी। वास्तव में मानव प्रेम धर्म जाति संप्रदाय और संकीर्णता पर नहीं टिका है।
लहना सिंह इलाके का हिस्ट्रीशीटर भी था; पर भगवान ने उसे गला इतना मीठा दिया था कि उसकी आवाज सुनने के लिए लोग दूर-दूर से आते थे। स्वयं थाने के लोग भी उसे बिठाकर फिल्मी गीत सुना करते थे। नामी चोर होते हुए भी लहना सिंह का अंदाज चाल ढाल किसी मस्ताने हीरो से कम न थी।
इसी संग्रह से
अपनी बात
चार नायिकाओं से सामना
प्रस्तुत कथा-संग्रह में लगभग छः दशक पुराने द्वितीय विश्वयुद्ध (१९३९-४५) और प्रथम विश्वयुद्ध (१९१४-१८) के मध्य काल की भारतीय जीवन की सामाजिक स्थितियों और घटनाओं को दरशाती चार
नायिकाओं की चार कहानियाँ हैं। पहली कहानी तप और योग साधना से निर्मित
हिमालय की योगिनी रमा की है। वह जीवन की आरंभिक अभावपूर्ण स्थितियों के
कारण विवाह न हो पाने की स्थिति में घर छोड़ कर तपस्वनी बनती है। गुरू
चेले की परंपरा में कुछ आत्मज्ञान पाकर ज्ञान योग के शीर्ष पर पहुंच कर
दिव्य शक्ति बन जाती है। नारी हृदय कोमल है। वह पुनः उसी पुरूष के
आमने-सामने होती है जो पहले उसका पति बनने वाला था। संयोग से वह भी साधु
होकर उन्हीं गुरू के पास जा पहुँचता है, जो रमा के पहले से ही गुरू हैं।
दोनों पति-पत्नी तो न बन सके, पर रमा गुरूभाई बनाकर उसके साथ देशाटन पर
निकल जाती है।
दूसरी कहानी की नायिका एक शिक्षित विधवा कृष्णा कुमारी है, जिसका मायका मुंबई में और ससुराल लखनऊ के पास नूतनपुर गाँव में है। वह विधवा अपने भाई के पास मुंबई में रहती है, जहाँ अतरपुर (लखनऊ) के जमींदार का पुत्र रमाकांत घर से पलायन कर मुंबई आ जाता है और कृष्णा कुमारी के आतिथ्य में रहता है। कृष्णा कुमारी ही कहानी की नायिका है और इसका प्यार का नाम ‘निन्ना दीदी’ है। काल के घटनाक्रम में रमाकांत पुनः जमींदार बनकर मुंबई की लड़की राजो से विवाह कर अतरपुर आ बसता है। नूतनपुर भी अतरपुर की जमींदारी का हिस्सा है। कृष्णा कुमारी की ससुराल की जमीन को एक दुष्ट कारिंदा हड़पना चाहता है, जिसे बचाने के लिए कृष्णा मुंबई से नूतनपुर और अतरपुर आती है। यह पता लगने पर कि जमींदार रमाकांत वही लड़का है, जो उसके यहाँ अतिथि और बच्चों का मास्टर था, वह स्वाभिमानिनी उससे दया की भीख माँगने की अपेक्षा मरना पसंद करती है। कहानी का उपसंहार दुःखांत पर प्रेरणाप्रद है। आज कितनी निन्ना दीदी है देश में !
तीसरी कहानी की नायिका एंग्लो-इंडियन नारी साँफी डेनियल है, जो जेम्स नामक ईसाई युवक से प्रेम-विवाह असफल होने पर उसके अत्याचार से घबराकर भाग लेती है और रेलवे के एक बड़े बाबू शर्माजी के पास शरण लेती है। मध्य प्रदेश का आज का नीमच शहर द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान वायसराय की रिजर्व पुलिस और रेलवे मिलिटरी ट्रेनिंग कैंप का मुख्यालय था। यहीं शर्माजी लार्ड बियर्ड साहब के साथ ड्यूटी क्लर्क थे। साँफी शर्माजी के परिवार की अनुपस्थिति में उनके साथ पत्नी बनकर रहती है और हिन्दुस्तानी संस्कृति को अपना लेती है। इस नायिका की भी सफल प्रेम के बिछोह की दर्दनाक दुःखांत कहानी है, जो तत्कालीन हिंदू समाज और ईसाई समाज के सामंजस्य को उभारकर सामने लाती है।
ये तीनों कहानियाँ लंबी हैं, पर चौथी कहानी की नायिका गाँव की गुर्जरी प्यारी है। वह हीर-राँझा गाने वाले लहना सिंह के गाँव में ब्याहकर आती है और अपने पति मंगू के शहरी दोस्त से आमना-सामना होने पर अपनी अल्हड़ता दिखाते हुए उचित और सभ्य व्यवहार कर कहानी में अपने चरित्र की छाप छोड़ती है। इस कहानी की नायिका प्यारी सदियों पुरानी गुर्जर संस्कृति की बीसवीं सदी की सजग और सजीव प्रतीक है और पूर्ण अशिक्षित होकर भी नारी-तेज से ओत-प्रोत है।
कहानी के गठन और बनाव-सिंगार में कितना सच होता और कितनी कल्पना, इसका सही अंदाज पाठक नहीं लगा पाते। इन कहानियों के पात्रों के चरित्र एवं घटनाक्रम के अनोखे मोड़ के प्रति आकर्षित रहें, इसे मैं सफल कहानी की कसौटी मानता हूँ।
दूसरी कहानी की नायिका एक शिक्षित विधवा कृष्णा कुमारी है, जिसका मायका मुंबई में और ससुराल लखनऊ के पास नूतनपुर गाँव में है। वह विधवा अपने भाई के पास मुंबई में रहती है, जहाँ अतरपुर (लखनऊ) के जमींदार का पुत्र रमाकांत घर से पलायन कर मुंबई आ जाता है और कृष्णा कुमारी के आतिथ्य में रहता है। कृष्णा कुमारी ही कहानी की नायिका है और इसका प्यार का नाम ‘निन्ना दीदी’ है। काल के घटनाक्रम में रमाकांत पुनः जमींदार बनकर मुंबई की लड़की राजो से विवाह कर अतरपुर आ बसता है। नूतनपुर भी अतरपुर की जमींदारी का हिस्सा है। कृष्णा कुमारी की ससुराल की जमीन को एक दुष्ट कारिंदा हड़पना चाहता है, जिसे बचाने के लिए कृष्णा मुंबई से नूतनपुर और अतरपुर आती है। यह पता लगने पर कि जमींदार रमाकांत वही लड़का है, जो उसके यहाँ अतिथि और बच्चों का मास्टर था, वह स्वाभिमानिनी उससे दया की भीख माँगने की अपेक्षा मरना पसंद करती है। कहानी का उपसंहार दुःखांत पर प्रेरणाप्रद है। आज कितनी निन्ना दीदी है देश में !
तीसरी कहानी की नायिका एंग्लो-इंडियन नारी साँफी डेनियल है, जो जेम्स नामक ईसाई युवक से प्रेम-विवाह असफल होने पर उसके अत्याचार से घबराकर भाग लेती है और रेलवे के एक बड़े बाबू शर्माजी के पास शरण लेती है। मध्य प्रदेश का आज का नीमच शहर द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान वायसराय की रिजर्व पुलिस और रेलवे मिलिटरी ट्रेनिंग कैंप का मुख्यालय था। यहीं शर्माजी लार्ड बियर्ड साहब के साथ ड्यूटी क्लर्क थे। साँफी शर्माजी के परिवार की अनुपस्थिति में उनके साथ पत्नी बनकर रहती है और हिन्दुस्तानी संस्कृति को अपना लेती है। इस नायिका की भी सफल प्रेम के बिछोह की दर्दनाक दुःखांत कहानी है, जो तत्कालीन हिंदू समाज और ईसाई समाज के सामंजस्य को उभारकर सामने लाती है।
ये तीनों कहानियाँ लंबी हैं, पर चौथी कहानी की नायिका गाँव की गुर्जरी प्यारी है। वह हीर-राँझा गाने वाले लहना सिंह के गाँव में ब्याहकर आती है और अपने पति मंगू के शहरी दोस्त से आमना-सामना होने पर अपनी अल्हड़ता दिखाते हुए उचित और सभ्य व्यवहार कर कहानी में अपने चरित्र की छाप छोड़ती है। इस कहानी की नायिका प्यारी सदियों पुरानी गुर्जर संस्कृति की बीसवीं सदी की सजग और सजीव प्रतीक है और पूर्ण अशिक्षित होकर भी नारी-तेज से ओत-प्रोत है।
कहानी के गठन और बनाव-सिंगार में कितना सच होता और कितनी कल्पना, इसका सही अंदाज पाठक नहीं लगा पाते। इन कहानियों के पात्रों के चरित्र एवं घटनाक्रम के अनोखे मोड़ के प्रति आकर्षित रहें, इसे मैं सफल कहानी की कसौटी मानता हूँ।
शक्ति त्रिवेदी
तेजस्विनी
प्रथम विश्वयुद्ध को समाप्त हुए अठारह
वर्ष बीत गए। सन् १९३६ आ गया। यूरोप और एशिया के देश अपनी सेनाओं का
पुनर्गठन कर रहे थे कि कहीं दुबारा महायुद्ध न छिड़ जाए। पहले युद्ध में
भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना में भरती होकर लड़े थे। अनेक योद्धाओं ने
‘विक्टोरिया क्रॉस’ भी जीते। इस समय भरतपुर एक जाट
राजा की छोटी सी रियासत थी। आज का उत्तर प्रदेश तब युक्त प्रांत कहलाता
था, जिसे अंग्रेजी भी कहते थे। और अंग्रेजी में तरक्की भी थी; महँगाई भी।
इस समय तक चाय, चीनी और डालडा का चलन हो चुका था। पर भरतपुर रियासत में
शुद्ध अन्न एवं दूध-घी सस्ता था। प्रजा गरीब थी। क्रय शक्ति न के बराबर
थी। कहीं-कहीं प्रजामंडल के आंदोलन चलते थे। आजादी की लड़ाई राजाओं के
विरूद्ध थी। जाटों का बोलबाला था। भरतपुर में लगभग सभी ओहदों पर जाट ही
नियुक्त थे। हरिजनों पर अत्याचार हो रहे थे। बेगार प्रथा से सभी त्रस्त
थे।
जन-जीवन अज्ञानी और भयभीत था। पुरूष नारियों पर भी जुल्म करते थे। राजा के सामने बनिए धोती की लाँग खोलकर, जमीन पर लेटकर नजर भेंट करते थे। खेतों में पैदावार कम थी। हर साल अकाल-सा पड़ता था। खेत मजदूर तो आधे पेट ही रहते थे। भूखे किसान-मजदूर प्रजामंडल (कांग्रेस) के नेताओं से गुहार करते थे कि वे जल्दी-जल्दी आंदोलन छेड़ें और उन्हें जेल ले चलें। वहाँ भरपेट रोटी तो मिलेगी। तब अपनी विधवा माँ का मैं ही एकमात्र पुत्र था।
सन् १९१४ की लड़ाई के समय मेरे पिता कामवन पहाड़ी (भरतपुर राज्य की तहसील) में पुलिस दारोगा थे। वे तांत्रिक व मांत्रिक भी थे। राजा जसवंत सिंह ने उन्हें बुलवाकर थानेदारी सौंपी थी। पहा़ड़ी में जहाँ मेवात की ओर डकैत आते थे वहाँ नई पुलिस चौकी खोल दी गई। उन्हें ऊँट और तलवार देकर चाँदी के दो रुपए महीने तनख्वाह तय कर दारोगा बना दीया गया। उस समय एस. पी. अंग्रेज ही होता था, भारतीय नहीं। लंबे संमय तक थानेदारी करके सन् १९१२ में जिन्न और प्रेतों से लड़ते हुए तंत्र विधान में उनकी अकाल मृत्यु हो गई। तब मैं डेढ़ वर्ष का था। हमारे दुःख के दिन शुरू हो गए। राजा ने मेरे पिता के सम्मान के नाते मुझे रियासत के अंग्रेजी स्कूल में मुफ्त दाखिला दे दिया। मैंने पाँच वर्ष की आयु से अठारह वर्ष की आयु तक उर्दू, हिंदी व अंग्रेजी पढ़ी। जब नवीं कक्षा में फेल हुआ तो वजीफा बंद होने पर पढ़ाई छूट गई। इसी बीच नगर (मेवात) से विवाह हुआ और पुत्र जनमा। उस समय नौकरी मिलना आज की तरह बहुत कठिन था। सभी दफ्तरों में चक्कर काटने पर भी मुझे नौकरी न मिल सकी। आर्थिक तंगी बढ़ने लगी। माँ और बीवी का क्रोध तथा झल्लाहट रोज ही सुनने को मिलती थी। हर शाम क्लेश होना चर्या बन चुका था।
रोज की तरह आज भी माँ का कर्कश स्वर फिर सुनाई पड़ने लगा, ‘‘दुनिया कमा के खा रही है और इसे कहीं काम ही नहीं मिलता। न जाने इसे कोई क्या लाट साब बना देगा। छोटी-मोटी नौकरी करते शर्म लगती है कुमार को !’’ और भी न जाने क्या-क्या बक रही थी। मैं चुपचाप सुनता रहा। नौकरी न मिलना मेरी लाचारी थी। क्या करता।
मैं चुपचाप बाहर पड़ी चारपाई पर बैठ गया। भूख जोर की लग रही थी, पर अब न जाने कहाँ गायब हो गई। फिर भी आशा थी कि माँ कुछ-न-कुछ खाना तो देगी ही। पर माँ व पत्नी में से कोई भी नहीं उठी।
मैंने कुछ समय तो प्रतीक्षा की। जब कोई हलचल न देखी तो चुपचाप ऊपर छत पर चला गया। खुली छत पर ही लेट गया। सोचा—आज शायद रोटी बनी ही न होगी। सोचने लगा—‘क्या किया जाए ? रोजगार की समस्या कैसे हल करूँ ?’ मैं जानता था कि मेरे पिता पुलिस के दारोगा थे। पिता जी के समय के कमाए हुए पाँच हजार रुपए माँ के पास थे। घर का खर्च मुश्किल से दस रुपए महीना था। पिताजी का जब देहांत हुआ तब मैं डेढ़ वर्ष का था और आज बीस वर्ष का हूँ। मेरी माँ घर में ही मजदूरी करके अपना और मेरा पेट पालती रही। पढाई भी कराई। सोलह साल का होते ही मेरा विवाह भी कर दिया। आज एक वर्ष का बच्चा भी गोद में है। विवाह और पुत्र जन्म संस्कार में माँ ने पाँच हजार रुपयों में से चार सौ रुपए खर्च भी कर दिये। हमारा वंश चलने लगा। बाकी माँ के पास जमा था, जिसे वह खर्च नहीं करना चाहती थी। विक्टोरिया के चाँदी के सिक्के माँ ने दीवारों में छुपा रखे थे। मैंने उसे मजदूरी करने से भी रोक दिया। मैं जवान हो गया, बाल-बच्चेवाला भी। बैठे-बैठे खाने से तो कुएँ भी खाली हो जाते हैं। वह धन ही कब तक चलेगा। बड़ी विकट समस्या थी।
सोचते-सोचते आँखें लग गई। दीये जल गए। छत पर अँधेरा बढ़ गया था। सहसा कानों में आवाज आई, ‘‘नीचे आ जा बेशरम ! नखरे और दिखाता है हमें। कितनी आवाजें मारी, पर सुनता ही नहीं !’’ आवाज माँ की थी। चुपचाप नीचे उतर आया। आँगन में पड़ी चारपाई पर सिर नीचा करके बैठ गया। चारपाई पर थाली में सब्जी और दो रोटियाँ रखी थीं। उसे देखते ही न जाने कहाँ से फिर भूख आ गई। खाने लगा चोर की तरह।
माँ भी नीचे बैठ गई और उसी रौद्र मुद्रा में बोली, ‘‘कहाँ गया था रे ?’’
‘‘टहलने!’’ मुख में अभी एक ग्रास ही चल रहा था।
‘‘बड़े टहलनेवाले बने हो ! आवारा घूमने से पेट नहीं भरेगा। कुछ कमाने की चिंता करो।’’
‘‘मैं आज डिप्टी साब के यहाँ भी गया था। उन्होंने कहा है कि अभी जगह खाली नहीं है। वहीं से टहलने निकल गया।’’ मैंने एक कौर निगलते हुए कहा।
‘‘जाने क्या आग लग गई है नौकरियों को ! भगवान ने एक ही औलाद दी है, वह भी बेकार निकम्मी ! लोगों के चार-चार बेटे हैं, सब कामों पर लगे हुए हैं। हमारा ही भाग्य क्यों उतना खोटा है !’’ कहकर माँ नें लंबी साँस ली और चुप हो गई। मैंने दूसरी रोटी भी खा ली और उठ गया।
यह किस्सा आज का नहीं, रोजाना का था। काम की खोज में फिरते-फिरते महीनों बीत गए, पर भाग्य ने साथ नहीं दीया। जिले के सभी दफ्तर, कारखाने, फर्मों, तक के चक्कर काट लिए। कहीं कोई रोजगार न मिल सका। मेरी असफलता का कारण यह भी था कि मैं ‘नाँन मैट्रिक’ था। कभी-कभी कोई ट्यूशन मिल जाता, कभी छूट जाता। पढ़ाई छोड़ने के बाद से दो वर्ष हो गए। कभी दस-बीस रुपए कमा लिये, कभी बेकार हो गया।
माँ का रोना भी ठीक था। मैं अकेला होता तो कोई बात न थी। पत्नी और बच्चा भी थे। बच्चे के दूध, ग्राइप वाटर, कपड़े और कुछ-न-कुछ खर्चा लगा ही रहता था। गनीमत थी कि कच्चा-पक्का सा मकान अपना था। माँ बेचारी कब तक खिलाती।
पत्नी अशिक्षिता पर मेहनती थी। वह ठेठ मेवाती, असंस्कृत और गोरी सुंदर व सुडौल थी। एक मन पक्का अनाज हाथ की चक्की पर पीस लेती थी। क्लेश होने पर काम छोड़ कर बैठ जाती। दिनभर खाना न खाती। कोठे में चारपाई पर लेट जाती या किसी कोनें में घंटों बैठ जाती। बच्चे को दूध भी न पिलाती। बेचारा रो-रोकर अपनी दादी के पास जाता। वही उसे खिला-पिलाकर, नहा-धुलाकर, कपड़े बदलकर अपने ही पास सुला लेती। माँ का चित्त मेरी पत्नी की ओर से भी खिन्न रहता था। पत्नी पर आया गुस्सा भी मेरे ऊपर उतरता।
मैं इकलौता बेटा था, लाड़-प्यार से पाला हुआ, आँखों का तारा। वह मुझे अपनी आँखों से दूर नौकरी के लिए कतई बाहर भेजना न चाहती थी। यह भी विचित्र परेशानी थी। शहर में रोजगार नहीं, बाहर जाने न दे।
पलायन
रात चाँदनी थी। हलकी ठंड पड़ रही थी। घर की छत पर पड़े गृहस्थ के क्लेश और नित्य की झक-झक से छुटकारा पाने के विचार हृदय में उठ रहे थे। माता, पिता, बच्चा, घर-मकान—सबकी ओर से मोह कम होता जा रहा था। संसार झूठा, बेईमान, स्वार्थी सा लग रहा था।
न जाने क्यों यही विचार मुझे बार-बार प्रेरित कर रहा था कि मैं घर छोड़कर कहीं चला जाऊँ। यदि वहाँ कोई काम मिल गया तो अपने गृहस्थ का निर्वाह करके जीवन को आगे धकेल ले जाऊँगा, अन्यथा कहीं भी भूखा-प्यासा रहकर प्राण ही त्याग दूँगा। शीघ्र ही उठा। नीचे आँगन में आकर देखा, सभी घोर निद्रा में सोए थे।
कुछ आवश्यक चीजें अटैची में रखकर चुपचाप चोर की तरह द्वार खोलकर घर से बाहर हो गया। सीधा स्टेशन की ओर चल पडा। प्लेटफाँर्म पर जाकर एक बेंच पर जा बैठा। स्टेशन पर सन्नाटा था। कुछ यात्री जमीन पर बिस्तर लगाए सो रहे थे। एक ओर कुछ रेलवे कर्मचारी बैठे चिलम पी रही थे। तारघर में एक बाबू बैठा खट-खट कर रहा था। कहीं कोई गाड़ी न थी। सोचने लगा—‘कहाँ जाऊँ ?’ मन ने फिर कहा—‘जो भी गाड़ी आए उसी में बैठ जाओ। कहीं तो पहुँच ही जाओगे, परंतु टिकट को पैसे कहाँ हैं ? सोचा। ‘बेटिकट ही चलो। जो होगा, देखा जाएगा।’ मन ने उत्तर दिया।
रेलवे कर्मचारी ने घंटा बजाया। हृदय धक-धक करने लगा। कई सोते हुए यात्री उठ बैठ गए। किसी ने पूछा, ‘‘कौन सी गाड़ी आ रही है ?’’
‘‘नाइंटीन डाउन।’’
‘‘क्या बजा है ?’’
‘‘पौने तीन।’’
कर्मचारी स्टेशन मास्टर के कमरे में घुस गया। यात्री बराबर में सोई एक महिला को जगाते हुए बोला, ‘‘उठो, दिल्ली एक्सप्रेस आ रही है। बिस्तर समेट लो।’’
महिला ने कसकर अँग़ड़ाई ली और बिस्तर बाँधने लगी।
फिर एक घंटा बजा। आस-पास सोने वाले सभी यात्री जाग पड़े। प्लेटफार्म पर रोशनी हो गई। दैत्य की भाँति धड़धड़ाती हुई ‘देहली एक्सप्रेस’ प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हो गई। खोमचेवाले शोर मचाने लगे—‘चाय गरम’, ‘पान-बीड़ी-सिगरेट’, ‘पूड़ी-साग’ वगैरह-वगैरह। यात्री गाड़ी की खिड़कियों को खुलवाकर जल्दी-जल्दी घुसने लगे। इधर-उधर भाग-दौड़ मच गई। मैं भी चुपचाप एक डिब्बे में जाकर बैठ गया। दिल धड़क रहा था।
गार्ड ने सीटी दी और इंजन हौंक उठा। गाड़ी चल दी। मन में बे-टिकट होने का भय था। पर कोई उपाय न था। जेब में एक पैसा न था। सोचने लगा—कभी-कभी विवश-असहाय की रक्षा ईश्वर करता है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। गाड़ी मथुरा स्टेशन पर आकर रुकी। ऊपर की एक बर्थ खाली हो गई। मैं उसी पर जाकर चुपचाप लेट गया। जब उठा तो सबेरा हो गया था। गाड़ी भी खड़ी थी। उतर कर देखा तो विद्युत्-प्रकाश जगमगा रहा था। किसी से पूछा, ‘‘कौन सा स्टेशन है?’’
‘‘दिल्ली !’’
मैं चुपचाप गाड़ी से उतरकर चल पड़ा। सोचने लगा—‘बाहर कैसे निकलूँ।’ रेलवे के डाकघर में आर-पार द्वार खुला था। लोग चिठ्ठी छाँटकर बोरे बाँधने में लगे थे। चुपके से निकलकर बाहर हो गया। अब मन को शांति मिली।
दिल्ली को देखने का यह मेरा पहला अवसर था। चौंका देने वाली भीड़, सरसराती हुई दौड़नेवाली मोटरों की भों-भों, खड़खड़ाती हुई ट्रामों की टन-टन, ‘हटो बाबू ! बचो बाबू ! भाईजी ! ओलाला !’ ताँगेवालों के तीखे स्वर, दौड़ लगाते हुए हाथ रिक्शा—ये सब मेरे लिए नई चीजें थीं। मैं इन्हें देखने को कहीं-कहीं खड़ा हो जाता। बड़े ध्यान से देखता। मन को आनंद मिलता, पर मन में अभाव सा खटकता। वह इसलिए कि यहाँ आकर मैं क्या करूँगा ? कहाँ से खाऊँगा ? कहाँ रहूँगा ? सहसा ध्यान आया—मामाजी ! हाँ, मेरी माँ के चाचा के लड़कों में से बीच वाले भाई थे—पं. कृष्णदत्तजी ! इत्तफाक से उनका पता मेरी नोट बुक में लिखा था। नोट-बुक निकालकर उसे पढ़ा—‘श्याम भवन, जाँनसन रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली।’ नई दिल्ली ? यह क्या कोई और दिल्ली है ? एक रिक्शे वाले से पूछा, ‘‘क्यों भाई, ये करोल बाग, नई दिल्ली किधर है ?’’
‘‘बैठो बाबू ! बारह आने देना।’’ उसने कहा।
‘‘कितनी दूर है यहाँ से ?’’ मैंने पूछा।
‘‘लगभग चार मील।’’
‘‘रास्ता किधर से है, बता सकोगे?’’ मैंने पूछा।
‘‘क्या पैदल ही जाओगे ? बहुत दूर है। चलो, दस आने देना।’’ रिक्शावाले ने कहा।
‘‘नहीं भाई, मुझे रास्ता ही बता दो।’’
‘‘जैसी मरजी ! यहाँ से सीधे चले जाओ, फतेहपुरी मसजिद आएगी। दाहिने मुड़ जाना, फिर खारी बावली होते हुए लाहौरी गेट, फिर सदर और बाड़ा हिन्दूराव पार कर बाएँ मुड़ जाना बस वहीं पूछ लेना।’’
मैं चल दिया। सब स्थानों को पार कर करोल बाग पहुँच गया। वहाँ पूछताछ कर जाँनसन रोड और श्याम भवन भी पहुँच गया। अंदर जाकर पं. कृष्णदत्त वकील को पूछा। वह दाहीने हाथ को ऊपर वाले भाग में रहते थे।
सीढियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचा तो मामी मिली। उनको नमस्ते कर मामाजी को पूछा। वह वहीं मौजूद थे। अंदर एक कमरे में उनका आँफिस था। उनको नमस्ते कर चरण-स्पर्श किए।
मुझे अचानक आया देख उन्होंने आश्चर्य से पूछा, ‘‘अरे तुम ! कब आए ?’’
‘‘जी, अभी चला ही आ रहा हूँ।’’
‘‘कौन सी गाड़ी से आए हो ?’’
‘‘दिल्ली एक्सप्रेस से !’’
‘‘तो वह तो सात बजे ही आ जाती है।’’ उन्होंने घड़ी देखकर कहा, ‘‘अब तो ग्यारह बजे हैं ?’’
‘‘जी हाँ ! मैं तो घूमते हुआ पैदल ही चला आ रहा हूँ।’’
‘‘ओह !’’ कुछ मुस्कराकर उन्होंने कहा।
मुझे खड़ा देखकर कुरसी की ओर इशारा कर बोले, ‘‘अरे, बैठो न। खड़े क्यों हो ?’’
मैं बैठ गया और उनके कमरे की सजावट को देखने लगा। वह बीच में कुरसी पर बैठे थे। सामने एक बड़ी टेबल थी। उस पर बहुत से कागज, किताबें, अखबार, शीशे के कलमदान और सुंदर कलमें। दो रंगीन शीशे के फूलदानों में ताजा फूल रखे थे। वह सिगरेट पीते थे। सिगरटों की एक चमकती डिब्बी और सिगरेट की राख झाड़ने का डिब्बा भी रखा था। सामने चार आलमारियों में किताबें भरी थीं। दाएँ-बाएँ खिड़कियाँ और दरवाजा था, जिन पर फूलदार छीट के रेशमी परदे लटके थे। दीवारों पर कलेंडर टँगे थे। हिन्दुस्तान का एक बड़ा नक्शा भी लटका हुआ था। यह सभी सजावट मुझे अच्छी लगी। मैंने आज तक ऐसे सुंदर, सजे हुए कमरे को देखा न था।
मामाजी कुछ लिखने लग गए। मैं बैठा-बैठा इन सबको देखता रहा। सहसा उन्होंने चश्मे को आँखों से माथे पर चढा कर मेरी ओर देखकर कहा, ‘‘मुन्ना, नहा-धोकर खाना खा लो। तुम्हारा नाम तो मैं भूल ही गया !’’
‘‘जी, नवीन !’’ मैंने बताया।
‘‘हाँ-हाँ, नवीन ! जीजी (बहन) तो ठीक है न ?’’
‘‘जी हाँ !’’
‘‘यहाँ अचानक कैसे चले आए ? पत्र तो डाल दीया होता !’’ उन्होंने मुस्कराकर पूछा।
इसका मैंने कोई उत्तर नहीं दिया।
उन्होंने फिर पूछा, ‘‘क्या कर रहे हो आजकल ?’’
‘‘जी, बेकार हूँ।’’
‘‘कहाँ तक पढे हो ?’’ मेरी ओर देखकर उन्होंने पूछा।
‘‘नवाँ पास कर स्कूल छोड़ दिया।’’
‘‘ओफ ! यह क्या किया ? मैट्रिक तो कर लिया होता !’’ वह फिर कुछ लिखने लग गए। मैं नहाने के लिए बाहर जाने को खड़ा हो गया। मुझे देखकर उन्होंने पुकारा, ‘‘लेखराज !’’
मेरी ही उम्र का एक युवक आकर बोला, ‘‘जी !’’
उसे बिना देखे ही मामाजी ने आदेश दिया, ‘‘देखो ! नवीन को बाथरूम बता दो और नहा धो लेने पर खाना खिला दो।’’
लेखराज ने मेरी ओर देखकर कहा, ‘‘आइए !’’
मैं उसके पीछे-पीछे चला गया।
‘बाथरूम’ एक सुंदर सफेद कमरा था। नीचे चिकने, चमकदार टाइल लगे थे। एक ओर नल था। ऊपर फव्वारा था। खूँटी पर तौलिया टँगा था। दीवार में एक चौकोर शीशा लगा था। उसके नीचे साबुन, तेल, कंघा रखे थे।
नहा-धोकर कपडे पहन, बालों में कंघा कर मैं बाहर आ गया। मुझे बड़ा आनंद आ रहा था इस समय। मामाजी ने मुझे खाने के लिए रसोई में बुला लिया वहाँ रसोइए ने टेबल पर खाना लगा दिया। मैं लज्जित सा वहाँ बैठ गया और खाने लगा। खाने में आलू-टमाटर, आलू-बैंगन, मटर-गोभी की सब्जी; चटनी-प्याज, उड़द की दाल और चावल-रोटी थे।
उनके लिए यह नित्य का साधारण भोजन था। मेरे लिए ये चीजें नई थीं। मैंने प्याज भी पहले कभी नहीं खाई थी। आज खा ही ली ! स्वाद भी लगी।
पीछे से मामीजी ने आकर कहा, ‘‘लल्ला, चावल के साथ चीनी भी ले लेना ! गाँव में तो चावल बूरे के साथ खातें हैं। वहाँ दाल-सब्जी से कोई नहीं खाता।’’
जन-जीवन अज्ञानी और भयभीत था। पुरूष नारियों पर भी जुल्म करते थे। राजा के सामने बनिए धोती की लाँग खोलकर, जमीन पर लेटकर नजर भेंट करते थे। खेतों में पैदावार कम थी। हर साल अकाल-सा पड़ता था। खेत मजदूर तो आधे पेट ही रहते थे। भूखे किसान-मजदूर प्रजामंडल (कांग्रेस) के नेताओं से गुहार करते थे कि वे जल्दी-जल्दी आंदोलन छेड़ें और उन्हें जेल ले चलें। वहाँ भरपेट रोटी तो मिलेगी। तब अपनी विधवा माँ का मैं ही एकमात्र पुत्र था।
सन् १९१४ की लड़ाई के समय मेरे पिता कामवन पहाड़ी (भरतपुर राज्य की तहसील) में पुलिस दारोगा थे। वे तांत्रिक व मांत्रिक भी थे। राजा जसवंत सिंह ने उन्हें बुलवाकर थानेदारी सौंपी थी। पहा़ड़ी में जहाँ मेवात की ओर डकैत आते थे वहाँ नई पुलिस चौकी खोल दी गई। उन्हें ऊँट और तलवार देकर चाँदी के दो रुपए महीने तनख्वाह तय कर दारोगा बना दीया गया। उस समय एस. पी. अंग्रेज ही होता था, भारतीय नहीं। लंबे संमय तक थानेदारी करके सन् १९१२ में जिन्न और प्रेतों से लड़ते हुए तंत्र विधान में उनकी अकाल मृत्यु हो गई। तब मैं डेढ़ वर्ष का था। हमारे दुःख के दिन शुरू हो गए। राजा ने मेरे पिता के सम्मान के नाते मुझे रियासत के अंग्रेजी स्कूल में मुफ्त दाखिला दे दिया। मैंने पाँच वर्ष की आयु से अठारह वर्ष की आयु तक उर्दू, हिंदी व अंग्रेजी पढ़ी। जब नवीं कक्षा में फेल हुआ तो वजीफा बंद होने पर पढ़ाई छूट गई। इसी बीच नगर (मेवात) से विवाह हुआ और पुत्र जनमा। उस समय नौकरी मिलना आज की तरह बहुत कठिन था। सभी दफ्तरों में चक्कर काटने पर भी मुझे नौकरी न मिल सकी। आर्थिक तंगी बढ़ने लगी। माँ और बीवी का क्रोध तथा झल्लाहट रोज ही सुनने को मिलती थी। हर शाम क्लेश होना चर्या बन चुका था।
रोज की तरह आज भी माँ का कर्कश स्वर फिर सुनाई पड़ने लगा, ‘‘दुनिया कमा के खा रही है और इसे कहीं काम ही नहीं मिलता। न जाने इसे कोई क्या लाट साब बना देगा। छोटी-मोटी नौकरी करते शर्म लगती है कुमार को !’’ और भी न जाने क्या-क्या बक रही थी। मैं चुपचाप सुनता रहा। नौकरी न मिलना मेरी लाचारी थी। क्या करता।
मैं चुपचाप बाहर पड़ी चारपाई पर बैठ गया। भूख जोर की लग रही थी, पर अब न जाने कहाँ गायब हो गई। फिर भी आशा थी कि माँ कुछ-न-कुछ खाना तो देगी ही। पर माँ व पत्नी में से कोई भी नहीं उठी।
मैंने कुछ समय तो प्रतीक्षा की। जब कोई हलचल न देखी तो चुपचाप ऊपर छत पर चला गया। खुली छत पर ही लेट गया। सोचा—आज शायद रोटी बनी ही न होगी। सोचने लगा—‘क्या किया जाए ? रोजगार की समस्या कैसे हल करूँ ?’ मैं जानता था कि मेरे पिता पुलिस के दारोगा थे। पिता जी के समय के कमाए हुए पाँच हजार रुपए माँ के पास थे। घर का खर्च मुश्किल से दस रुपए महीना था। पिताजी का जब देहांत हुआ तब मैं डेढ़ वर्ष का था और आज बीस वर्ष का हूँ। मेरी माँ घर में ही मजदूरी करके अपना और मेरा पेट पालती रही। पढाई भी कराई। सोलह साल का होते ही मेरा विवाह भी कर दिया। आज एक वर्ष का बच्चा भी गोद में है। विवाह और पुत्र जन्म संस्कार में माँ ने पाँच हजार रुपयों में से चार सौ रुपए खर्च भी कर दिये। हमारा वंश चलने लगा। बाकी माँ के पास जमा था, जिसे वह खर्च नहीं करना चाहती थी। विक्टोरिया के चाँदी के सिक्के माँ ने दीवारों में छुपा रखे थे। मैंने उसे मजदूरी करने से भी रोक दिया। मैं जवान हो गया, बाल-बच्चेवाला भी। बैठे-बैठे खाने से तो कुएँ भी खाली हो जाते हैं। वह धन ही कब तक चलेगा। बड़ी विकट समस्या थी।
सोचते-सोचते आँखें लग गई। दीये जल गए। छत पर अँधेरा बढ़ गया था। सहसा कानों में आवाज आई, ‘‘नीचे आ जा बेशरम ! नखरे और दिखाता है हमें। कितनी आवाजें मारी, पर सुनता ही नहीं !’’ आवाज माँ की थी। चुपचाप नीचे उतर आया। आँगन में पड़ी चारपाई पर सिर नीचा करके बैठ गया। चारपाई पर थाली में सब्जी और दो रोटियाँ रखी थीं। उसे देखते ही न जाने कहाँ से फिर भूख आ गई। खाने लगा चोर की तरह।
माँ भी नीचे बैठ गई और उसी रौद्र मुद्रा में बोली, ‘‘कहाँ गया था रे ?’’
‘‘टहलने!’’ मुख में अभी एक ग्रास ही चल रहा था।
‘‘बड़े टहलनेवाले बने हो ! आवारा घूमने से पेट नहीं भरेगा। कुछ कमाने की चिंता करो।’’
‘‘मैं आज डिप्टी साब के यहाँ भी गया था। उन्होंने कहा है कि अभी जगह खाली नहीं है। वहीं से टहलने निकल गया।’’ मैंने एक कौर निगलते हुए कहा।
‘‘जाने क्या आग लग गई है नौकरियों को ! भगवान ने एक ही औलाद दी है, वह भी बेकार निकम्मी ! लोगों के चार-चार बेटे हैं, सब कामों पर लगे हुए हैं। हमारा ही भाग्य क्यों उतना खोटा है !’’ कहकर माँ नें लंबी साँस ली और चुप हो गई। मैंने दूसरी रोटी भी खा ली और उठ गया।
यह किस्सा आज का नहीं, रोजाना का था। काम की खोज में फिरते-फिरते महीनों बीत गए, पर भाग्य ने साथ नहीं दीया। जिले के सभी दफ्तर, कारखाने, फर्मों, तक के चक्कर काट लिए। कहीं कोई रोजगार न मिल सका। मेरी असफलता का कारण यह भी था कि मैं ‘नाँन मैट्रिक’ था। कभी-कभी कोई ट्यूशन मिल जाता, कभी छूट जाता। पढ़ाई छोड़ने के बाद से दो वर्ष हो गए। कभी दस-बीस रुपए कमा लिये, कभी बेकार हो गया।
माँ का रोना भी ठीक था। मैं अकेला होता तो कोई बात न थी। पत्नी और बच्चा भी थे। बच्चे के दूध, ग्राइप वाटर, कपड़े और कुछ-न-कुछ खर्चा लगा ही रहता था। गनीमत थी कि कच्चा-पक्का सा मकान अपना था। माँ बेचारी कब तक खिलाती।
पत्नी अशिक्षिता पर मेहनती थी। वह ठेठ मेवाती, असंस्कृत और गोरी सुंदर व सुडौल थी। एक मन पक्का अनाज हाथ की चक्की पर पीस लेती थी। क्लेश होने पर काम छोड़ कर बैठ जाती। दिनभर खाना न खाती। कोठे में चारपाई पर लेट जाती या किसी कोनें में घंटों बैठ जाती। बच्चे को दूध भी न पिलाती। बेचारा रो-रोकर अपनी दादी के पास जाता। वही उसे खिला-पिलाकर, नहा-धुलाकर, कपड़े बदलकर अपने ही पास सुला लेती। माँ का चित्त मेरी पत्नी की ओर से भी खिन्न रहता था। पत्नी पर आया गुस्सा भी मेरे ऊपर उतरता।
मैं इकलौता बेटा था, लाड़-प्यार से पाला हुआ, आँखों का तारा। वह मुझे अपनी आँखों से दूर नौकरी के लिए कतई बाहर भेजना न चाहती थी। यह भी विचित्र परेशानी थी। शहर में रोजगार नहीं, बाहर जाने न दे।
पलायन
रात चाँदनी थी। हलकी ठंड पड़ रही थी। घर की छत पर पड़े गृहस्थ के क्लेश और नित्य की झक-झक से छुटकारा पाने के विचार हृदय में उठ रहे थे। माता, पिता, बच्चा, घर-मकान—सबकी ओर से मोह कम होता जा रहा था। संसार झूठा, बेईमान, स्वार्थी सा लग रहा था।
न जाने क्यों यही विचार मुझे बार-बार प्रेरित कर रहा था कि मैं घर छोड़कर कहीं चला जाऊँ। यदि वहाँ कोई काम मिल गया तो अपने गृहस्थ का निर्वाह करके जीवन को आगे धकेल ले जाऊँगा, अन्यथा कहीं भी भूखा-प्यासा रहकर प्राण ही त्याग दूँगा। शीघ्र ही उठा। नीचे आँगन में आकर देखा, सभी घोर निद्रा में सोए थे।
कुछ आवश्यक चीजें अटैची में रखकर चुपचाप चोर की तरह द्वार खोलकर घर से बाहर हो गया। सीधा स्टेशन की ओर चल पडा। प्लेटफाँर्म पर जाकर एक बेंच पर जा बैठा। स्टेशन पर सन्नाटा था। कुछ यात्री जमीन पर बिस्तर लगाए सो रहे थे। एक ओर कुछ रेलवे कर्मचारी बैठे चिलम पी रही थे। तारघर में एक बाबू बैठा खट-खट कर रहा था। कहीं कोई गाड़ी न थी। सोचने लगा—‘कहाँ जाऊँ ?’ मन ने फिर कहा—‘जो भी गाड़ी आए उसी में बैठ जाओ। कहीं तो पहुँच ही जाओगे, परंतु टिकट को पैसे कहाँ हैं ? सोचा। ‘बेटिकट ही चलो। जो होगा, देखा जाएगा।’ मन ने उत्तर दिया।
रेलवे कर्मचारी ने घंटा बजाया। हृदय धक-धक करने लगा। कई सोते हुए यात्री उठ बैठ गए। किसी ने पूछा, ‘‘कौन सी गाड़ी आ रही है ?’’
‘‘नाइंटीन डाउन।’’
‘‘क्या बजा है ?’’
‘‘पौने तीन।’’
कर्मचारी स्टेशन मास्टर के कमरे में घुस गया। यात्री बराबर में सोई एक महिला को जगाते हुए बोला, ‘‘उठो, दिल्ली एक्सप्रेस आ रही है। बिस्तर समेट लो।’’
महिला ने कसकर अँग़ड़ाई ली और बिस्तर बाँधने लगी।
फिर एक घंटा बजा। आस-पास सोने वाले सभी यात्री जाग पड़े। प्लेटफार्म पर रोशनी हो गई। दैत्य की भाँति धड़धड़ाती हुई ‘देहली एक्सप्रेस’ प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हो गई। खोमचेवाले शोर मचाने लगे—‘चाय गरम’, ‘पान-बीड़ी-सिगरेट’, ‘पूड़ी-साग’ वगैरह-वगैरह। यात्री गाड़ी की खिड़कियों को खुलवाकर जल्दी-जल्दी घुसने लगे। इधर-उधर भाग-दौड़ मच गई। मैं भी चुपचाप एक डिब्बे में जाकर बैठ गया। दिल धड़क रहा था।
गार्ड ने सीटी दी और इंजन हौंक उठा। गाड़ी चल दी। मन में बे-टिकट होने का भय था। पर कोई उपाय न था। जेब में एक पैसा न था। सोचने लगा—कभी-कभी विवश-असहाय की रक्षा ईश्वर करता है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। गाड़ी मथुरा स्टेशन पर आकर रुकी। ऊपर की एक बर्थ खाली हो गई। मैं उसी पर जाकर चुपचाप लेट गया। जब उठा तो सबेरा हो गया था। गाड़ी भी खड़ी थी। उतर कर देखा तो विद्युत्-प्रकाश जगमगा रहा था। किसी से पूछा, ‘‘कौन सा स्टेशन है?’’
‘‘दिल्ली !’’
मैं चुपचाप गाड़ी से उतरकर चल पड़ा। सोचने लगा—‘बाहर कैसे निकलूँ।’ रेलवे के डाकघर में आर-पार द्वार खुला था। लोग चिठ्ठी छाँटकर बोरे बाँधने में लगे थे। चुपके से निकलकर बाहर हो गया। अब मन को शांति मिली।
दिल्ली को देखने का यह मेरा पहला अवसर था। चौंका देने वाली भीड़, सरसराती हुई दौड़नेवाली मोटरों की भों-भों, खड़खड़ाती हुई ट्रामों की टन-टन, ‘हटो बाबू ! बचो बाबू ! भाईजी ! ओलाला !’ ताँगेवालों के तीखे स्वर, दौड़ लगाते हुए हाथ रिक्शा—ये सब मेरे लिए नई चीजें थीं। मैं इन्हें देखने को कहीं-कहीं खड़ा हो जाता। बड़े ध्यान से देखता। मन को आनंद मिलता, पर मन में अभाव सा खटकता। वह इसलिए कि यहाँ आकर मैं क्या करूँगा ? कहाँ से खाऊँगा ? कहाँ रहूँगा ? सहसा ध्यान आया—मामाजी ! हाँ, मेरी माँ के चाचा के लड़कों में से बीच वाले भाई थे—पं. कृष्णदत्तजी ! इत्तफाक से उनका पता मेरी नोट बुक में लिखा था। नोट-बुक निकालकर उसे पढ़ा—‘श्याम भवन, जाँनसन रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली।’ नई दिल्ली ? यह क्या कोई और दिल्ली है ? एक रिक्शे वाले से पूछा, ‘‘क्यों भाई, ये करोल बाग, नई दिल्ली किधर है ?’’
‘‘बैठो बाबू ! बारह आने देना।’’ उसने कहा।
‘‘कितनी दूर है यहाँ से ?’’ मैंने पूछा।
‘‘लगभग चार मील।’’
‘‘रास्ता किधर से है, बता सकोगे?’’ मैंने पूछा।
‘‘क्या पैदल ही जाओगे ? बहुत दूर है। चलो, दस आने देना।’’ रिक्शावाले ने कहा।
‘‘नहीं भाई, मुझे रास्ता ही बता दो।’’
‘‘जैसी मरजी ! यहाँ से सीधे चले जाओ, फतेहपुरी मसजिद आएगी। दाहिने मुड़ जाना, फिर खारी बावली होते हुए लाहौरी गेट, फिर सदर और बाड़ा हिन्दूराव पार कर बाएँ मुड़ जाना बस वहीं पूछ लेना।’’
मैं चल दिया। सब स्थानों को पार कर करोल बाग पहुँच गया। वहाँ पूछताछ कर जाँनसन रोड और श्याम भवन भी पहुँच गया। अंदर जाकर पं. कृष्णदत्त वकील को पूछा। वह दाहीने हाथ को ऊपर वाले भाग में रहते थे।
सीढियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचा तो मामी मिली। उनको नमस्ते कर मामाजी को पूछा। वह वहीं मौजूद थे। अंदर एक कमरे में उनका आँफिस था। उनको नमस्ते कर चरण-स्पर्श किए।
मुझे अचानक आया देख उन्होंने आश्चर्य से पूछा, ‘‘अरे तुम ! कब आए ?’’
‘‘जी, अभी चला ही आ रहा हूँ।’’
‘‘कौन सी गाड़ी से आए हो ?’’
‘‘दिल्ली एक्सप्रेस से !’’
‘‘तो वह तो सात बजे ही आ जाती है।’’ उन्होंने घड़ी देखकर कहा, ‘‘अब तो ग्यारह बजे हैं ?’’
‘‘जी हाँ ! मैं तो घूमते हुआ पैदल ही चला आ रहा हूँ।’’
‘‘ओह !’’ कुछ मुस्कराकर उन्होंने कहा।
मुझे खड़ा देखकर कुरसी की ओर इशारा कर बोले, ‘‘अरे, बैठो न। खड़े क्यों हो ?’’
मैं बैठ गया और उनके कमरे की सजावट को देखने लगा। वह बीच में कुरसी पर बैठे थे। सामने एक बड़ी टेबल थी। उस पर बहुत से कागज, किताबें, अखबार, शीशे के कलमदान और सुंदर कलमें। दो रंगीन शीशे के फूलदानों में ताजा फूल रखे थे। वह सिगरेट पीते थे। सिगरटों की एक चमकती डिब्बी और सिगरेट की राख झाड़ने का डिब्बा भी रखा था। सामने चार आलमारियों में किताबें भरी थीं। दाएँ-बाएँ खिड़कियाँ और दरवाजा था, जिन पर फूलदार छीट के रेशमी परदे लटके थे। दीवारों पर कलेंडर टँगे थे। हिन्दुस्तान का एक बड़ा नक्शा भी लटका हुआ था। यह सभी सजावट मुझे अच्छी लगी। मैंने आज तक ऐसे सुंदर, सजे हुए कमरे को देखा न था।
मामाजी कुछ लिखने लग गए। मैं बैठा-बैठा इन सबको देखता रहा। सहसा उन्होंने चश्मे को आँखों से माथे पर चढा कर मेरी ओर देखकर कहा, ‘‘मुन्ना, नहा-धोकर खाना खा लो। तुम्हारा नाम तो मैं भूल ही गया !’’
‘‘जी, नवीन !’’ मैंने बताया।
‘‘हाँ-हाँ, नवीन ! जीजी (बहन) तो ठीक है न ?’’
‘‘जी हाँ !’’
‘‘यहाँ अचानक कैसे चले आए ? पत्र तो डाल दीया होता !’’ उन्होंने मुस्कराकर पूछा।
इसका मैंने कोई उत्तर नहीं दिया।
उन्होंने फिर पूछा, ‘‘क्या कर रहे हो आजकल ?’’
‘‘जी, बेकार हूँ।’’
‘‘कहाँ तक पढे हो ?’’ मेरी ओर देखकर उन्होंने पूछा।
‘‘नवाँ पास कर स्कूल छोड़ दिया।’’
‘‘ओफ ! यह क्या किया ? मैट्रिक तो कर लिया होता !’’ वह फिर कुछ लिखने लग गए। मैं नहाने के लिए बाहर जाने को खड़ा हो गया। मुझे देखकर उन्होंने पुकारा, ‘‘लेखराज !’’
मेरी ही उम्र का एक युवक आकर बोला, ‘‘जी !’’
उसे बिना देखे ही मामाजी ने आदेश दिया, ‘‘देखो ! नवीन को बाथरूम बता दो और नहा धो लेने पर खाना खिला दो।’’
लेखराज ने मेरी ओर देखकर कहा, ‘‘आइए !’’
मैं उसके पीछे-पीछे चला गया।
‘बाथरूम’ एक सुंदर सफेद कमरा था। नीचे चिकने, चमकदार टाइल लगे थे। एक ओर नल था। ऊपर फव्वारा था। खूँटी पर तौलिया टँगा था। दीवार में एक चौकोर शीशा लगा था। उसके नीचे साबुन, तेल, कंघा रखे थे।
नहा-धोकर कपडे पहन, बालों में कंघा कर मैं बाहर आ गया। मुझे बड़ा आनंद आ रहा था इस समय। मामाजी ने मुझे खाने के लिए रसोई में बुला लिया वहाँ रसोइए ने टेबल पर खाना लगा दिया। मैं लज्जित सा वहाँ बैठ गया और खाने लगा। खाने में आलू-टमाटर, आलू-बैंगन, मटर-गोभी की सब्जी; चटनी-प्याज, उड़द की दाल और चावल-रोटी थे।
उनके लिए यह नित्य का साधारण भोजन था। मेरे लिए ये चीजें नई थीं। मैंने प्याज भी पहले कभी नहीं खाई थी। आज खा ही ली ! स्वाद भी लगी।
पीछे से मामीजी ने आकर कहा, ‘‘लल्ला, चावल के साथ चीनी भी ले लेना ! गाँव में तो चावल बूरे के साथ खातें हैं। वहाँ दाल-सब्जी से कोई नहीं खाता।’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book