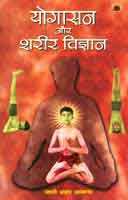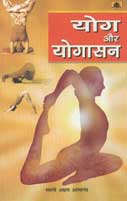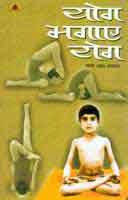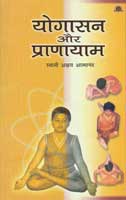|
योग >> योगासन और शरीर विज्ञान योगासन और शरीर विज्ञानस्वामी अक्षय आत्मानन्द
|
430 पाठक हैं |
||||||
इसमें योगासन और शरीर विज्ञान संबंधी अनेक उपयोगी जानकारियाँ...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
इस पुस्तक में योगासन और शरीर विज्ञान सम्बन्धी अनेक उपयोगी जानकारियाँ दी
गई हैं। चित्रों सहित विषय को समझने की सर्वथा एक नवीन शैली प्रस्तुति
इसलिए उपयुक्त लगेगी कि आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार पढ़-समझ सकेंगे।
पुस्तक में योगासनों के साथ-साथ कुछ ऐसी सामग्रियों का भी समावेश किया गया है, जिनके मनन मात्र से आपका जीवन असीम कार्य क्षमता और आनन्दमय उल्लास से भर उठेगा।
अति सरल भाषा, विशिष्ट शैली, गम्भीर वैज्ञानिक विश्लेषण और सुबोध व्याख्या स्वामी अक्षय आत्मानंदजी की पुस्तकों की ऐसी विशेषताएँ हैं, जिनमें पाठक उनकी योग सम्बन्धी पुस्तकों को रुचिपूर्वक पढ़ते हैं।
योग-जगत के अति श्रद्धास्पद अधिकारी गुरु के रूप में प्रख्यात स्वामी अक्षय आत्मानंद द्वारा योगासन, प्राणायाम, अध्यात्म विज्ञान, सम्मोहन विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान आदि पर अत्यन्त सरल-सुबोध भाषा एवं तार्किक शैली में अति रोचक एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की गई है। स्वामी जी का साहित्य इतना लोकप्रिय हुआ है कि उनके ग्रन्थों के कई-कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं।
पुस्तक में योगासनों के साथ-साथ कुछ ऐसी सामग्रियों का भी समावेश किया गया है, जिनके मनन मात्र से आपका जीवन असीम कार्य क्षमता और आनन्दमय उल्लास से भर उठेगा।
अति सरल भाषा, विशिष्ट शैली, गम्भीर वैज्ञानिक विश्लेषण और सुबोध व्याख्या स्वामी अक्षय आत्मानंदजी की पुस्तकों की ऐसी विशेषताएँ हैं, जिनमें पाठक उनकी योग सम्बन्धी पुस्तकों को रुचिपूर्वक पढ़ते हैं।
योग-जगत के अति श्रद्धास्पद अधिकारी गुरु के रूप में प्रख्यात स्वामी अक्षय आत्मानंद द्वारा योगासन, प्राणायाम, अध्यात्म विज्ञान, सम्मोहन विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान आदि पर अत्यन्त सरल-सुबोध भाषा एवं तार्किक शैली में अति रोचक एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की गई है। स्वामी जी का साहित्य इतना लोकप्रिय हुआ है कि उनके ग्रन्थों के कई-कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं।
एक संन्यासी की पुकार
हमारा शरीर चूँकि प्रकृति के मूल तत्त्वों से निर्मित है, अत: यह जड़
पदार्थ है। जड़ पदार्थों के अस्तित्व एवं प्राकृतिक व्यवस्थाओं का एक क्रम
है। यह क्रम प्रारंभ होना, यह क्रम समाप्त होना, इसकी आयु उन
पदार्थों के समघटन पर निर्भर करता है। यह बात शरीर-विज्ञान और
शारीरिक संचरना से, उसके प्रस्तुतीकरण के ढंग से शायद आप समझ जाएंगे। आप
यह तो अवश्य ही समझ जाएँगे कि शरीर जन्म लेता है तो मरता भी अवश्य है;
परन्तु आत्मा नामक यात्री ही उसे आबाद करता है और बरबाद होते देख उसे
छोड़कर भाग खड़ा होता है।
शरीर आत्मा का आधार है, पड़ाव है, विश्रामस्थल है, मंजिल नहीं। फिर भी मंजिल मिलने तक उसे इस आधार की अवश्यकता है। रुकने और विश्राम करने की, अपने आपको तरोताजा करने की, अपनी हँसी-खुशी, स्वास्थ्य-सुविधा बनाए रखने की उसे महती आवश्यकता है, ताकि वह एक दिन अपनी मंजिल पा सके।
इस ग्रंथ में शरीर-विज्ञान, योगासन के अनेक आसन व अनेक जानकारियाँ दी गई हैं। अनेक खंडों में, टुकड़े-टुकड़े कर सम्पूर्ण ज्ञान इसलिए प्रस्तुत करना पड़ रहा है कि आप इसे रुक-रुककर पढ़ें, इसका मनन करें, इसका पालन कर सकने का संकल्प लें। यदि आप पाठकों में से दो-चार को भी मंजिल मिल सकी तो मेरा श्रम सार्थक होगा।
ग्रंथ आप पढ़ेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे; परन्तु निस्संदेह अनेक ऐसे स्थल आएँगे, जहाँ या तो आप ठीक से समझ न पा रहे होंगे अथवा मेरे सीमित शब्द ही अपनी भावाभिव्यक्ति ठीक से नहीं कर पा रहे होंगे। इस अवरोध को दूर करने के लिए आप मुझसे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं। यदि आप लोग अधिक संख्या में हैं, एक ही स्थान पर हैं, एकत्रित हैं, तो मुझे भी बुला सकते हैं। निश्चित पता और समय कृपया प्रकाशक से ही पूछें।
महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को पूरा समझा पाने के लिए मैंने इन ग्रन्थों को आठ खंड़ों में बाँटने का संकल्प किया है। यदि इस बीच मेरे स्नेही पाठक अधिक शंकाएँ कर बैठे तो समाधान करने में संभवत: एक-दो खंड और भी बढ़ सकते हैं। वैसे आठ अंगों के लिएआठ खंड ठीक ही रहेंगे। आपको को भी स्वतंत्रता होगी कि आप इनमें से किसी भी पड़ाव को अपनी मंजिल बना लें।
अंत में एक बात और कहना चाहूँगा, वह यह है कि ‘योग’ भारत का अविष्कार है। भारतीय योगियों ने समय-समय पर इस ‘योग-विज्ञान’ को सरल और बहुजन-हितकारी बनाने के लिए नए-नए प्रयोग भी किए हैं। प्रत्येक प्रयोग से उत्तम निष्कर्ष निकाले हैं। खेद हैं तो सिर्फ इस बात का कि उन ऋषियों की संतान, हम भारतवासी उन निष्कर्षों को सँभाल नहीं पाएँ; उनकी ओर पर्याप्त रुचि, लगन और निष्ठा नहीं दिखा पाए। फलस्वरूप हमारी वर्तमान पीढ़ी हमारे पूर्वजों द्वारा संगृहीत अमूल्य संपदा की उत्तराधिकारिणी नहीं बन पाई।
मैंने इधर अनेक गूढ़ रहस्यों को पुन: खोज निकाला है। उन्हें प्रयोग की कसौटी पर कसकर आधुनिक परिवेश भी दिया है। अब मुझे खोज है सिर्फ उन योग्य पात्रों की, उन ट्रस्टियों की, जो इस ज्ञान को पीढ़ी-दर-पीढ़ी सौंपते जाएँ; कुछ उदारमना सज्जनों की, जो नई खोजों के लिए मुझे सहयोग दे सकें, साधन दे सकें, संरक्षण दे सकें। क्या कोई मेरी आवाज़ सुनेगा ?
शरीर आत्मा का आधार है, पड़ाव है, विश्रामस्थल है, मंजिल नहीं। फिर भी मंजिल मिलने तक उसे इस आधार की अवश्यकता है। रुकने और विश्राम करने की, अपने आपको तरोताजा करने की, अपनी हँसी-खुशी, स्वास्थ्य-सुविधा बनाए रखने की उसे महती आवश्यकता है, ताकि वह एक दिन अपनी मंजिल पा सके।
इस ग्रंथ में शरीर-विज्ञान, योगासन के अनेक आसन व अनेक जानकारियाँ दी गई हैं। अनेक खंडों में, टुकड़े-टुकड़े कर सम्पूर्ण ज्ञान इसलिए प्रस्तुत करना पड़ रहा है कि आप इसे रुक-रुककर पढ़ें, इसका मनन करें, इसका पालन कर सकने का संकल्प लें। यदि आप पाठकों में से दो-चार को भी मंजिल मिल सकी तो मेरा श्रम सार्थक होगा।
ग्रंथ आप पढ़ेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे; परन्तु निस्संदेह अनेक ऐसे स्थल आएँगे, जहाँ या तो आप ठीक से समझ न पा रहे होंगे अथवा मेरे सीमित शब्द ही अपनी भावाभिव्यक्ति ठीक से नहीं कर पा रहे होंगे। इस अवरोध को दूर करने के लिए आप मुझसे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं। यदि आप लोग अधिक संख्या में हैं, एक ही स्थान पर हैं, एकत्रित हैं, तो मुझे भी बुला सकते हैं। निश्चित पता और समय कृपया प्रकाशक से ही पूछें।
महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को पूरा समझा पाने के लिए मैंने इन ग्रन्थों को आठ खंड़ों में बाँटने का संकल्प किया है। यदि इस बीच मेरे स्नेही पाठक अधिक शंकाएँ कर बैठे तो समाधान करने में संभवत: एक-दो खंड और भी बढ़ सकते हैं। वैसे आठ अंगों के लिएआठ खंड ठीक ही रहेंगे। आपको को भी स्वतंत्रता होगी कि आप इनमें से किसी भी पड़ाव को अपनी मंजिल बना लें।
अंत में एक बात और कहना चाहूँगा, वह यह है कि ‘योग’ भारत का अविष्कार है। भारतीय योगियों ने समय-समय पर इस ‘योग-विज्ञान’ को सरल और बहुजन-हितकारी बनाने के लिए नए-नए प्रयोग भी किए हैं। प्रत्येक प्रयोग से उत्तम निष्कर्ष निकाले हैं। खेद हैं तो सिर्फ इस बात का कि उन ऋषियों की संतान, हम भारतवासी उन निष्कर्षों को सँभाल नहीं पाएँ; उनकी ओर पर्याप्त रुचि, लगन और निष्ठा नहीं दिखा पाए। फलस्वरूप हमारी वर्तमान पीढ़ी हमारे पूर्वजों द्वारा संगृहीत अमूल्य संपदा की उत्तराधिकारिणी नहीं बन पाई।
मैंने इधर अनेक गूढ़ रहस्यों को पुन: खोज निकाला है। उन्हें प्रयोग की कसौटी पर कसकर आधुनिक परिवेश भी दिया है। अब मुझे खोज है सिर्फ उन योग्य पात्रों की, उन ट्रस्टियों की, जो इस ज्ञान को पीढ़ी-दर-पीढ़ी सौंपते जाएँ; कुछ उदारमना सज्जनों की, जो नई खोजों के लिए मुझे सहयोग दे सकें, साधन दे सकें, संरक्षण दे सकें। क्या कोई मेरी आवाज़ सुनेगा ?
स्वामी अक्षय आत्मानन्द
योग, प्राण और शरीर-विज्ञान
इस ग्रन्थ का प्रथम भाग ‘योग और योगासन’ निस्संदेह आप
पढ़
चुके होंगे, उसी क्रम में योग की दूसरी कड़ी जोड़ते हुए कुछ विशिष्ट
जानकारियाँ इस ग्रंथ के माध्यम से आप तक पहुँचाई जा रही हैं। योग की
बारीकियाँ, योगासन की दैनिक विधियाँ, रोगों से बचाव और उपचार, प्राणायाम
की प्रारम्भिक जानकारियाँ तथा शरीर-विज्ञान की कुछ विशिष्ट जानकारियाँ
इसमें सम्मिलित हैं। प्रत्येक विषय अलग-अलग अध्याय में प्रस्तुत करना
हमारी विवशता है; जबकि इन सबको सम्मिलित रूप से जीवन में उतार देना आपके
लिए लाभदायक और आवश्यक है। स्मरण रखिए कि ये समस्त जानकारियाँ मानवमात्र
के लिए हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलकर पूर्ण
‘मानव’
बनता है। अत: महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए यह जानकारी है।
उपनिषद् के ऋषि कहते हैं- यह जगत् अनित्य है।
मानव भ्रमित है। उसके भ्रम का कारण यह है कि वह देखता कुछ है, पाता कुछ है, सोचता कुछ है और धर्मग्रन्थों, ऋषियों, मनीषियों की बातें तथा तथ्य सुनने में दूसरे ही सुनता है। उस बेचारे को विश्वास भी नहीं होता कि देखने और सुनने में इतना अंतर कैसे हो सकता है।
यदि जगत् अनित्य है, देह नश्वर है, रिश्ते-नाते, स्थितियाँ माया हैं तो फिर सत्य क्या है, नित्य क्या है, इस माया और जगत् में हमारा अस्तित्व ही क्यों है ?
नित्य उसे कहते हैं- जो सदा से ही था, आज भी है और सदा बना रहेगा। जिसके रूप, रंग, आकृति और स्थिति में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसका कभी कोई रूपांतरण भी नहीं होता। जो आज भी वैसा ही है जैसा सदा से था और सदा ऐसा ही बना रहेगा। निश्चित ही जगत् ऐसा नहीं है। जगत् अनित्य है। हमें लगता हैं कि यह ‘है’; परन्तु यह हर क्षण, प्रतिपल बदल रहा है, भागा जा रहा है।
एक निरंतर दौड़, एक तीव्र गत्यात्मकता, एक अव्यक्त सी क्षणभंगुरता, प्रतिपल परिवर्तनशीलता का ही दूसरा नाम जगत् है। फिर भी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा-यह क्रम कभी भंग नहीं होता। वह नहीं तो न सही, कुछ और सही, इनसे बहुत भ्रान्ति पैदा होती है। सभी वस्तुएँ लगती हैं कि ‘हैं’, शरीर भी लगता है कि ‘है’, संसार भी लगता है कि ‘है’। हम जब नहीं थे तब संसार था। हम इस संसार में ही हैं। हम नहीं रहेंगे तब भी संसार रहेगा, लोग रहेंगे। हम जो कुछ करते थे, उसे दूसरे लोग करेंगे। लेकिन इसे ही ‘होना’ कैसे कह सकते हैं ? यह तो एक धारा है, प्रवाह है।
नही है। जल का दो किनारों के बीच बहना ही नदी है। उसका अहर्निश वेग, प्रवाह ही उसे ‘नदी’ बनाता है। हम किनारे खड़े होकर नदी को देख रहे हैं, नदी बह रही है। हमारे देखते-देखते ही हजारों टन पानी बह गया। जो सामने था वह दूर जा चुका है। जो दूर था वह भी सामने आकर दूर, बहुत दूर चला जा रहा है।
हम नदी को देख रहे हैं, नदी के पानी को देख रहे हैं। यह पानी वही पानी नहीं है। जब वही पानी नहीं है तो वही नदी कैसे हो सकती है ?
उपनिषद् के ऋषि कहते हैं- यह जगत् अनित्य है।
मानव भ्रमित है। उसके भ्रम का कारण यह है कि वह देखता कुछ है, पाता कुछ है, सोचता कुछ है और धर्मग्रन्थों, ऋषियों, मनीषियों की बातें तथा तथ्य सुनने में दूसरे ही सुनता है। उस बेचारे को विश्वास भी नहीं होता कि देखने और सुनने में इतना अंतर कैसे हो सकता है।
यदि जगत् अनित्य है, देह नश्वर है, रिश्ते-नाते, स्थितियाँ माया हैं तो फिर सत्य क्या है, नित्य क्या है, इस माया और जगत् में हमारा अस्तित्व ही क्यों है ?
नित्य उसे कहते हैं- जो सदा से ही था, आज भी है और सदा बना रहेगा। जिसके रूप, रंग, आकृति और स्थिति में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसका कभी कोई रूपांतरण भी नहीं होता। जो आज भी वैसा ही है जैसा सदा से था और सदा ऐसा ही बना रहेगा। निश्चित ही जगत् ऐसा नहीं है। जगत् अनित्य है। हमें लगता हैं कि यह ‘है’; परन्तु यह हर क्षण, प्रतिपल बदल रहा है, भागा जा रहा है।
एक निरंतर दौड़, एक तीव्र गत्यात्मकता, एक अव्यक्त सी क्षणभंगुरता, प्रतिपल परिवर्तनशीलता का ही दूसरा नाम जगत् है। फिर भी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा-यह क्रम कभी भंग नहीं होता। वह नहीं तो न सही, कुछ और सही, इनसे बहुत भ्रान्ति पैदा होती है। सभी वस्तुएँ लगती हैं कि ‘हैं’, शरीर भी लगता है कि ‘है’, संसार भी लगता है कि ‘है’। हम जब नहीं थे तब संसार था। हम इस संसार में ही हैं। हम नहीं रहेंगे तब भी संसार रहेगा, लोग रहेंगे। हम जो कुछ करते थे, उसे दूसरे लोग करेंगे। लेकिन इसे ही ‘होना’ कैसे कह सकते हैं ? यह तो एक धारा है, प्रवाह है।
नही है। जल का दो किनारों के बीच बहना ही नदी है। उसका अहर्निश वेग, प्रवाह ही उसे ‘नदी’ बनाता है। हम किनारे खड़े होकर नदी को देख रहे हैं, नदी बह रही है। हमारे देखते-देखते ही हजारों टन पानी बह गया। जो सामने था वह दूर जा चुका है। जो दूर था वह भी सामने आकर दूर, बहुत दूर चला जा रहा है।
हम नदी को देख रहे हैं, नदी के पानी को देख रहे हैं। यह पानी वही पानी नहीं है। जब वही पानी नहीं है तो वही नदी कैसे हो सकती है ?
हम हर क्षण मरते हैं, मरना ही जिंदगी है
आप सोचते हैं कि आप सिर्फ एक बार ही मरते हैं। नहीं, यह भूल है आपकी। आपके
पूरे जीवन में आप न जाने कितनी बार पूरे-के-पूरे मर जाते हैं। आपका यह
शरीर हजारों बार मर चुका है। दिन के प्रति सेकेंड में आपके शरीर के कई-कई
Cells, कई-कई कोशिकाएँ मरती हैं और हर पल शरीर के बाहर निकल जाती हैं।
यदि हम किसी शरीर-वैज्ञानिक से, किसी डॉक्टर से पूछें तो वह हमें समझाएगा, वह हमें बताएगा कि किस प्रकार हमारे शरीर का एक-एक टुकड़ा, एक-एक अणु प्रतिपल मर रहा है और शरीर के बाहर फिंक रहा है। हमारे शरीर में एक भी वह टुकड़ा या अणु शेष नहीं रह जाता, जो सात साल पहले था। सात साल में सब गल जाता है, सब बह जाता है और पूरा शरीर ही नया हो जाता है। बदल जाता है। जो आदमी सत्तर साल तक जीता है, वह अपने जीवन में दस बार पूरी तरह मर जाता है। दस बार नए शरीर के साथ नया जन्म ले लेता है। दस बार उनका शरीर पूरे तौर पर बदल जाता है। कमाल है कि सत्तर साल में दस बार दूसरा-दूसरा शरीरधारी होकर भी वह अपने इसी शरीर के द्वारा पहचाना जाता है !
शरीर की एक-एक कोशिका, मांसपेशी, हड्डी और चमड़ी बदल रही है, मर रही है। एक के मरते ही दूसरे का जन्म हो रहा है। हर क्षण शरीर खाली हो रहा है, हर क्षण शरीर मर रहा है। यह जो धारा है, यही जिंदगी भी है और मौत भी है। जब शरीर बदल रहा है, मर रहा है तो स्वास्थ्य भी नष्ट होगा ही।
आज तक जनमा शिशु कल बालक बन जाएगा। बचपन जवानी में बदल जाएगा। कल यह जवानी भी ढल जाएगी और बुढापा रोने-रुलाने पहुँच जाएगा। यह मत सोचना कि बचपन बुढ़ापे के विपरीत है। न मित्र, नहीं। यह तो उसी धारा का एक अंग है। इसी रक्त की सरिता में जन्म होता है। इसमें ही जवानी का घाट आता है और बुढ़ापे का घाट भी। और अंत में यह रक्त की सरिता एक दिन मृत्यु सागर में खो जाती है। जन्म ही मृत्यु का पहला कदम है और मृत्यु जन्म की आखिरी मंजिल है। यह शरीर, यह पहचान एक भ्रम है। जो तिल-तिलकर मरता जा रहा है, जो नहीं है फिर भी होने का भ्रम पैदा कर रहा है। मरते हुए आदमी को हम जिन्दा कहते हैं। मौत को जिंदगी मानते हैं। यही तो शरीर की नश्वरता है। यही तो जगत् की अनित्यता है।
नश्वरता, क्षणभंगुरता और अनित्यता पर हमारा इतना विश्वास है। इसे हम पकड़ लेने के, बाँध लेने के मनसूबे गाँठते हैं। अपने झूठे प्रयास कर इतराते हैं। अहंकार से बदले-बदले नजर आते हैं। एक क्षण मात्र का तो हमें पता नहीं और बड़ी-बड़ी बातें बघारते हैं।
यदि हम किसी शरीर-वैज्ञानिक से, किसी डॉक्टर से पूछें तो वह हमें समझाएगा, वह हमें बताएगा कि किस प्रकार हमारे शरीर का एक-एक टुकड़ा, एक-एक अणु प्रतिपल मर रहा है और शरीर के बाहर फिंक रहा है। हमारे शरीर में एक भी वह टुकड़ा या अणु शेष नहीं रह जाता, जो सात साल पहले था। सात साल में सब गल जाता है, सब बह जाता है और पूरा शरीर ही नया हो जाता है। बदल जाता है। जो आदमी सत्तर साल तक जीता है, वह अपने जीवन में दस बार पूरी तरह मर जाता है। दस बार नए शरीर के साथ नया जन्म ले लेता है। दस बार उनका शरीर पूरे तौर पर बदल जाता है। कमाल है कि सत्तर साल में दस बार दूसरा-दूसरा शरीरधारी होकर भी वह अपने इसी शरीर के द्वारा पहचाना जाता है !
शरीर की एक-एक कोशिका, मांसपेशी, हड्डी और चमड़ी बदल रही है, मर रही है। एक के मरते ही दूसरे का जन्म हो रहा है। हर क्षण शरीर खाली हो रहा है, हर क्षण शरीर मर रहा है। यह जो धारा है, यही जिंदगी भी है और मौत भी है। जब शरीर बदल रहा है, मर रहा है तो स्वास्थ्य भी नष्ट होगा ही।
आज तक जनमा शिशु कल बालक बन जाएगा। बचपन जवानी में बदल जाएगा। कल यह जवानी भी ढल जाएगी और बुढापा रोने-रुलाने पहुँच जाएगा। यह मत सोचना कि बचपन बुढ़ापे के विपरीत है। न मित्र, नहीं। यह तो उसी धारा का एक अंग है। इसी रक्त की सरिता में जन्म होता है। इसमें ही जवानी का घाट आता है और बुढ़ापे का घाट भी। और अंत में यह रक्त की सरिता एक दिन मृत्यु सागर में खो जाती है। जन्म ही मृत्यु का पहला कदम है और मृत्यु जन्म की आखिरी मंजिल है। यह शरीर, यह पहचान एक भ्रम है। जो तिल-तिलकर मरता जा रहा है, जो नहीं है फिर भी होने का भ्रम पैदा कर रहा है। मरते हुए आदमी को हम जिन्दा कहते हैं। मौत को जिंदगी मानते हैं। यही तो शरीर की नश्वरता है। यही तो जगत् की अनित्यता है।
नश्वरता, क्षणभंगुरता और अनित्यता पर हमारा इतना विश्वास है। इसे हम पकड़ लेने के, बाँध लेने के मनसूबे गाँठते हैं। अपने झूठे प्रयास कर इतराते हैं। अहंकार से बदले-बदले नजर आते हैं। एक क्षण मात्र का तो हमें पता नहीं और बड़ी-बड़ी बातें बघारते हैं।
जिसे हम नहीं जानते, वही हमारी पहचान है
जिस दिन हमारी मृत्यु-यात्रा प्रारम्भ होती है, उस क्षण को हम जन्म कहते
हैं; परन्तु मृत्यु को हम ‘जन्म’ कहने का साहस भी
नहीं जुटा
पाते। आज तो तुम्हारा दु:ख है, यदि वही किसी गरीब के पास होता तो वह उसका
सुख कहलाता। तुम्हारा आज जो सुख है, आनंद है वही अनेक क्रंदन है, दु:ख है।
फिर भी तुम सुख को दु:ख और दु:ख को सुख कहने से नहीं कतराते। तुम्हारी
मित्रता दूसरों की शत्रुता है। तुम्हारी शत्रुता दूसरों की मित्रता है।
मित्रता ही शत्रुता है और शत्रुता ही मित्रता है; पर यह तुम समझोगे कैसे
? तुम्हारा स्वास्थ्य दुनिया भर की सड़ाँध, बीमारियों और मौत से
जूझ
रहा है, फिर भी तुम भले-चंगे हो
?
?
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book