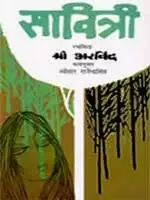|
पौराणिक >> सावित्री सावित्रीश्री अरविंद
|
297 पाठक हैं |
||||||
सावित्री के जीवन पर आधारित महाकाव्य...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
योगीराज श्री अरविन्द के प्रसिद्ध महाकाव्य ‘सावित्री’ का
गद्य में यह सरल हिन्दी भावानुवाद है जिसे हिन्दी के पुराने और प्रतिष्ठित
लेखक व्योहार राजेन्द्रसिंह ने प्रस्तुत किया है।
इस महत्त्वपूर्ण काव्य में सावित्री-सत्यवान की पुराण-कथा के माध्यम से कवि ने अपने दर्शन तथा इस पृथ्वी पर महामानव के अवतरण की अपनी विशिष्ट कल्पना को व्यक्त किया है। यह महाकाव्य बड़ा भी बहुत है, इसलिए मूल में इसका संपूर्ण वाचन और मनन सभी के लिए संभव नहीं है। इस भावानुवाद में संक्षेप में काव्य कथा और उसके भीतर निहित भावना, जितना संभव हो सकता था उतने सरल शब्दों में, सामान्य पाठकों के लिए प्रस्तुत की है।
मूल पाठक के बाद ‘सावित्री’ के कतिपय अंशों के कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा किये गये काव्यानुवाद ‘सावित्री’ की रचना-प्रक्रिया और विचार-भूमि से संदर्भित श्री अरविंद के पत्र तथा सावित्री का महत्त्व निरूपण करता श्री मां का वक्तव्य आदि बहुमूल्य-उपयोगी संदर्भ-सामग्री भी दे दी गई है, जिसमें यह पुस्तक स्थायी महत्त्व की ओर संग्रहणीय बन गई है।
इस महत्त्वपूर्ण काव्य में सावित्री-सत्यवान की पुराण-कथा के माध्यम से कवि ने अपने दर्शन तथा इस पृथ्वी पर महामानव के अवतरण की अपनी विशिष्ट कल्पना को व्यक्त किया है। यह महाकाव्य बड़ा भी बहुत है, इसलिए मूल में इसका संपूर्ण वाचन और मनन सभी के लिए संभव नहीं है। इस भावानुवाद में संक्षेप में काव्य कथा और उसके भीतर निहित भावना, जितना संभव हो सकता था उतने सरल शब्दों में, सामान्य पाठकों के लिए प्रस्तुत की है।
मूल पाठक के बाद ‘सावित्री’ के कतिपय अंशों के कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा किये गये काव्यानुवाद ‘सावित्री’ की रचना-प्रक्रिया और विचार-भूमि से संदर्भित श्री अरविंद के पत्र तथा सावित्री का महत्त्व निरूपण करता श्री मां का वक्तव्य आदि बहुमूल्य-उपयोगी संदर्भ-सामग्री भी दे दी गई है, जिसमें यह पुस्तक स्थायी महत्त्व की ओर संग्रहणीय बन गई है।
भूमिका
‘सावित्री’ श्री अरविन्द का महाकाव्य है जिसे उन्होंने अपने
आश्रम के एकान्तवास में लिखा था। उनकी अन्तिम रचना है। वैसे तो प्रारम्भ
काल से ही उन्होंने अंग्रेजी में कविता करने में दक्षता प्राप्त कर ली थी।
किन्तु आश्रम में उनका पूर्ण विकास हुआ। ‘सावित्री का कथानक
महाभारत
में 18 श्लोकों में दिया गया है। उसी का आधार लेकर उन्होंने 11 पर्वों और
41 सर्गों में यह महाकाव्य समाप्त किया है। इसमें 10 हजार
पंक्तियाँ
है। सावित्री ईश्वरीय कृपा की प्रतीक है जो कि सत्यवान रूपी जीव को ईश्वर
तक पहुँचाने के लिए अवतरित होती है। वह जीवात्मा को परमात्मा से मिलाकर और
फिर पृथ्वी पर वापस आकर स्वर्ग का राज्य स्थापित करती है। श्रीअरविन्द का
दावा है कि ‘सावित्री’ बौद्धिक नहीं, अन्तः प्रेरित
(intutional) काव्य है जिसकी कुछ पंक्तियाँ ही नहीं, पृष्ठ के
पृष्ठ
ईश्वरीय प्रेरणा से लिखे गए हैं।
प्रतीक काव्य
श्री अरविन्द ने कहा है कि मुझे ऐसा लगता था कि इसकी पंक्तियाँ ऊपर से
उतरती चली आ रही हैं और मुझसे लिखवाई जा रही हैं। सावित्री एक प्रतीकात्मक
काव्य है। साहित्य-समालोचक कहते हैं कि कवि की विशेष प्रतिभा बिम्बों का
सृजन करने में है। ये बिम्ब प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त होते जा रहे हैं
जो कवि की सर्जनात्मक प्रेरणा अथवा सृजन शक्ति के रूप में प्रकट होती है।
ये बिम्ब वहीं तक प्रभावशाली और यथार्थ होते हैं। जहाँ वे कवि के अनुभव या
उस चेतना की अवस्था को प्रकट करते हैं। जब ये बिम्ब यथार्थ होते हैं तब वे
प्रतीक बन जाते हैं। वह कविता केवल अनुभव मात्र नहीं रह जाती किन्तु
प्रभावशाली अभिव्यक्ति बन जाती है। श्री अरविन्द इसको ‘अनिवार्य
शब्द’ तथा ‘प्रेरक’ कहते हैं। अंग्रजी कवि
ए० ई० अपने
दर्शन के अनुभव को यथार्थ अप्रत्यक्ष मानते हैं। उसके सम्बन्ध में श्री
अरविन्द कहते हैं-‘‘दर्शन कवि की एक विशेष शक्ति है,
जिस
प्रकार विवेक तत्त्ववेत्ता का विशेष वरदान है और विश्लेषण वैज्ञानिक की
स्वाभाविक देन है।’’
यही दर्शन की शक्ति, अपने अनुभव के सत्य का दर्शन अथवा अतिमानस सत्य, जो कि प्रतीक के रूप में प्रकट होता है, कवि को आत्म-प्रकाशन की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए कवि सृजन करता है अथवा अपनी कल्पना से ऐसा बौद्धिक प्रतीक निर्माण करता है जो पाठकों को कवि का अभिप्रेत अर्थ समझाता है। कालिदास मेघ को दूत बनाकर और शैली स्काईलार्क पक्षी को प्रतीक बनाकर अपनी बात कहते हैं।
ये प्रतीक कैसे उत्पन्न होते हैं, यह कवियों, आलोचकों और मनोवैज्ञानिकों के लिए एक समस्या बन गई है। कुछ लोग इसकी उत्पत्ति अवचेतन और सामूहिक अचेतन से मानते हैं किन्तु उससे हमारा पूरा समाधान नहीं होता। दे लुई (Day Lewis) अपनी ‘पोयटिक इमेज’ (Poetic Image) नामक पुस्तक में कहते हैं कि काव्योप्तति की प्रणाली एक रहस्य है क्योंकि कवि की चेतना एक बहुत संश्लिष्ट वस्तु है। इसकी चेतना के अनेक स्तर होते हैं जिनमें काव्य का स्रोत रहता है। काव्यात्मक प्रतीक भी अनेक प्रकार के होते हैं और अनेक स्तरों पर दीख पड़ते हैं। जितने ऊँचे स्तर से वह प्रतीक देखा जाता है उतनी ही सार्थकता उसमें रहती है। जितने सम्बन्ध में श्रीअरविन्द ने लिखा है ‘‘प्रतीक अनेक प्रकार के होते हैं। प्रतीकों का अनेक प्रकार से बौद्धिक अर्थ किया जा सकता है।’’
जान बनियन की ‘पिल्ग्रिम्स प्रॉग्रेस’ एक रूपक है। शैली का ‘प्रॉमेथियस अनबाउण्ड’ भी इस प्रकार का रूपक है।
प्रतीक के कार्य के संबंध में श्रीअरविन्द एक जगह लिखते हैं—‘‘प्रतीक से कोई अव्यक्त वस्तु या विचार प्रकट नहीं होते अपितु एक जीवित सत्य, आन्तरिक दर्शन या अनुभव प्रकट होता है। यह दर्शन इतना सूक्ष्म होता है कि वह बौद्धिक अव्यक्त से भी परे होता है। प्रतीकात्मक बिम्बों के सिवा उसे व्यक्त करना कठिन होता है।’’
कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि प्रतीक प्राचीन कवियों के लिए ही उपयुक्त था, वह आधुनिक भावबोध के कवियों के उपयुक्त नहीं है। किन्तु तथ्य इसके विरूद्ध है। ब्लेक आदि प्राचीन कवियों ने ही प्रतीक का प्रयोग नहीं किया, वर्तमान कवियों ने भी इसका प्रयोग किया है। टामसन के ‘हाउण्ड’ आव हेवेन’ में दिव्य प्रेम आर मानव आत्मा का प्रतीकात्मक वर्णन है।
डल्ल्यू बी ईट्स और ए० ई० अपनी कविताओं और नाटकों में प्राचीन प्रतीकात्मक कथाओं का प्रचुर उपयोग किया करते हैं। लुई और हरबर्ट रीड के काव्य भी प्रतीकात्मक हैं। इसी परम्परा में श्रीअरविन्द की ‘सावित्री’ महान् काव्य हैं। ‘सावित्री’ के पहले भी उन्होंने बहुत-सी छोटी और बड़ी कविताएं लिखी थीं। जिनमें प्रतीकों का उपयोग किया गया था।
यही दर्शन की शक्ति, अपने अनुभव के सत्य का दर्शन अथवा अतिमानस सत्य, जो कि प्रतीक के रूप में प्रकट होता है, कवि को आत्म-प्रकाशन की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए कवि सृजन करता है अथवा अपनी कल्पना से ऐसा बौद्धिक प्रतीक निर्माण करता है जो पाठकों को कवि का अभिप्रेत अर्थ समझाता है। कालिदास मेघ को दूत बनाकर और शैली स्काईलार्क पक्षी को प्रतीक बनाकर अपनी बात कहते हैं।
ये प्रतीक कैसे उत्पन्न होते हैं, यह कवियों, आलोचकों और मनोवैज्ञानिकों के लिए एक समस्या बन गई है। कुछ लोग इसकी उत्पत्ति अवचेतन और सामूहिक अचेतन से मानते हैं किन्तु उससे हमारा पूरा समाधान नहीं होता। दे लुई (Day Lewis) अपनी ‘पोयटिक इमेज’ (Poetic Image) नामक पुस्तक में कहते हैं कि काव्योप्तति की प्रणाली एक रहस्य है क्योंकि कवि की चेतना एक बहुत संश्लिष्ट वस्तु है। इसकी चेतना के अनेक स्तर होते हैं जिनमें काव्य का स्रोत रहता है। काव्यात्मक प्रतीक भी अनेक प्रकार के होते हैं और अनेक स्तरों पर दीख पड़ते हैं। जितने ऊँचे स्तर से वह प्रतीक देखा जाता है उतनी ही सार्थकता उसमें रहती है। जितने सम्बन्ध में श्रीअरविन्द ने लिखा है ‘‘प्रतीक अनेक प्रकार के होते हैं। प्रतीकों का अनेक प्रकार से बौद्धिक अर्थ किया जा सकता है।’’
जान बनियन की ‘पिल्ग्रिम्स प्रॉग्रेस’ एक रूपक है। शैली का ‘प्रॉमेथियस अनबाउण्ड’ भी इस प्रकार का रूपक है।
प्रतीक के कार्य के संबंध में श्रीअरविन्द एक जगह लिखते हैं—‘‘प्रतीक से कोई अव्यक्त वस्तु या विचार प्रकट नहीं होते अपितु एक जीवित सत्य, आन्तरिक दर्शन या अनुभव प्रकट होता है। यह दर्शन इतना सूक्ष्म होता है कि वह बौद्धिक अव्यक्त से भी परे होता है। प्रतीकात्मक बिम्बों के सिवा उसे व्यक्त करना कठिन होता है।’’
कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि प्रतीक प्राचीन कवियों के लिए ही उपयुक्त था, वह आधुनिक भावबोध के कवियों के उपयुक्त नहीं है। किन्तु तथ्य इसके विरूद्ध है। ब्लेक आदि प्राचीन कवियों ने ही प्रतीक का प्रयोग नहीं किया, वर्तमान कवियों ने भी इसका प्रयोग किया है। टामसन के ‘हाउण्ड’ आव हेवेन’ में दिव्य प्रेम आर मानव आत्मा का प्रतीकात्मक वर्णन है।
डल्ल्यू बी ईट्स और ए० ई० अपनी कविताओं और नाटकों में प्राचीन प्रतीकात्मक कथाओं का प्रचुर उपयोग किया करते हैं। लुई और हरबर्ट रीड के काव्य भी प्रतीकात्मक हैं। इसी परम्परा में श्रीअरविन्द की ‘सावित्री’ महान् काव्य हैं। ‘सावित्री’ के पहले भी उन्होंने बहुत-सी छोटी और बड़ी कविताएं लिखी थीं। जिनमें प्रतीकों का उपयोग किया गया था।
आध्यात्मिक महाकाव्य
सावित्री शब्द ‘सवित्र’ से बना है। इसमें
‘सु’ धातु है जिसका अर्थ है, उत्पन्न करना। सोम शब्द
भी
‘सु’ धातु से बना है जिसका अर्थ है उत्साहवर्धन प्रेम
अथवा
आत्मिक आनन्द। इस प्रकार सावित्री का अर्थ है-सर्जक, सृष्टि को उत्पन्न
करने वाला। वेदों में सविता प्रकाश ओर सृजन का देवता है। उसका पार्थिव
प्रतीक हमारा सूर्य है जो समस्त सौरजगत को प्रकाशित और पोषित करता है।
इस प्रकार ‘सावित्री’ का अर्थ होगा-साविता की पुत्री अथवा दैवी सर्जक की शक्ति। ‘सावित्री’ महाकाव्य सावित्री दैवी का प्रतीक है, जो मानव रूप में अवतरित होकर मानवात्मा को अपने दैवी लक्ष्य की ओर ले जाती है। सत्यवान का अर्थ है- जिसके पास सत्य है अथवा जो सत्य पाना चाहता है। इस काव्य में सावित्री के पिता अश्वपति को जीवन-स्वामी माना गया है। वेदों में अश्व जीवनी शक्ति का द्योतक है, अतः अश्वपति का अर्थ जीवन का स्वामी ही हो सकता है। ‘सावित्री में राजा अश्वपति पृथ्वी पर अवतरित जिज्ञासु आत्मा का प्रतीक है।
सावित्री की कथा महाभारत अरण्य पर्व अ, 208 पर आधारित है। श्री अरविन्द ने वह कथा ज्यों की त्यों रक्खी है, केवल उसे प्रतीकात्मक बना दिया है, उसे जीवित प्रतीक में बदल दिया है। प्रथम पर्व के एक कोने से तीन सर्गों में कवि ने अपनी विश्व-सृजन सम्बन्धी मान्यता का वर्णन किया है। अश्वपति का चरित्र विश्व-सृजन सम्बन्धी मान्यता का वर्णन किया है। अश्वपति का चरित्र भी उसी में वर्णित है। सत्यवान के लिए अश्वपति की तपस्या को कवि ने आत्मज्ञान और विश्वज्ञान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासु मानवता की खोज के रूप में चित्रित किया गया है। द्वितीय पर्व में अश्वपति विश्व के विभिन्न स्तरों से ऊपर उठते हुए उच्चतर मानस तथा उच्च ज्ञान के स्तर तक पहुँच जाता है। उसके हदय में जिज्ञासा की अग्नि प्रज्ज्वलित है।
अश्वपति इस पृथ्वी पर सतयुग लाना चाहते हैं। मानव चेतना कितना महान ज्ञान अर्जित कर सकती है, वह कितनी गहराई और ऊँचाई तक जा सकती है, यह अश्वपति की तपस्या से प्रकट होता है। जितनी अधिक पूर्णता इस पृथ्वी पर लाना सम्भव है। उसकी प्राप्ति के लिए उसका हृदय छटपटाता है। तृतीय पर्व में अश्वपति विश्व के ऊपर प्रवेश कर अनुभव प्राप्त करता है और सृजनशक्ति के आमने-सामने पहुँच जाता है। वह आत्मा के दिव्य लोक के दर्शन करता है जहाँ सत्य शक्ति और चेतना दिव्य आनंद और समरसता एक साथ मौजूद हैं। वह इन सब तत्त्वों को पृथ्वी पर उतारना चाहता है, पृथ्वी पर दिव्य राज्य लाना चाहता है। दैवी शक्ति से उसे वरदान प्राप्त होता है कि अन्धकार व अज्ञान शक्तियों को जीतकर सत्य को मानव जगत् में उतार सके। दैवी शक्ति उसे वरदान देती है कि उसकी कृपा पृथ्वी पर अवतरित होगी।
इस प्रकार सावित्री का पृथ्वी पर जन्म होता है। सन्तान-कामना की एक सामान्य कथा को श्रीअरविन्द ने यह दिव्य रूप दिया है। अश्वपति की यात्रा अचेतन से चेतन के उच्च स्तर पर पहुँचने की यात्रा है। इसकी कठिनाई मानवात्वा द्वारा अनुभूत विघ्न-बाधाएँ हैं जो उसे सत्यवान की प्राप्ति में सामने आती हैं और उसकी सफलता मानव-जाति के द्वारा सत्य की प्राप्ति की सफलता है।
सावित्री भी केवल महाभारत की एक सामान्य राजकुमारी न रहकर दिव्य कृपा की अवतार बन जाती है। वह मानव के दुःखों और अपमानों को सहकर अन्धता और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर दिव्यलोक की प्राप्ति करती है। वह यमराज का सामना कर अपने पति सत्यवान को मृत्युपाश से छुड़ाती है। अपनी अमरता और अनन्तता के विस्तार से ही वह यह विजय प्राप्त करती है।
सावित्री का जन्म, बाल्यकाल, पति के वरण की उसकी यात्रा, सत्यवान से मिलन वापस आने पर नारद से मिलन आदि कथाएं ज्यों की त्यों रक्खी गई हैं। अन्तर इतना ही है कि श्रीअरविन्द की सावित्री अपनी मनुष्यता के साथ अपनी दिव्यता का भी एक साथ अनुभव करती है। नारद-सावित्री-संवाद में कवि ने विश्वनियन्ता का उद्देश्य तथा मानव के अदृश्य और कर्म सिद्धान्त को उच्च शिखर पर पहुँचा दिया है।
सावित्री के 4 से 6 पर्वों में दैवी माता द्वारा दिए गए वरदान की महत्ता प्रदर्शित की गई है। यम-सावित्री केवल मानव-जाति की प्रतिनिधि नहीं है। अपितु दैवी कृपा की भी अवतार है। यम कुटिलता, प्रलोभन, छल आदि को उपस्थिति करने वाले अज्ञान का प्रतिनिधि है। सारा संवाद उच्च के उच्चतर स्तर पर उठता चला जाता है। उसमें अतिमानस क्षेत्र की ज्योति और आत्मप्रेरणा की चमक बीच-बीच में कौंध जाती है।
एक छोटे-से कथानक को कितना विस्तृत और उच्च शिखर तक पहुँचाया जा सकता है, इसका प्रमाण है ‘सावित्री’ महाकाव्य। उसमें मनोवैज्ञानिक तथ्य भरे हुए हैं, जिससे मानव-विकास हो सकता है। महाकवि की यही उन्नयन कला है, जो मानवीय है। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सावित्री का प्राचीन कथानक समाप्त हो जाता है। पिता का राज्य प्राप्त कर सावित्री और सत्यवान राज्य-सुख भोगने लगते हैं। किंतु श्री अरविन्द की ‘सावित्री’ में वे दोनों मृत्यु का राज्य पार कर अन्नत दिवस के राज्य में प्रवेश करते हैं जहाँ कि सत्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, जहाँ अज्ञान और मृत्यु का कोई स्थान नहीं है। वहाँ कुछ काल ठहरकर वे दोनों पृथ्वी की ओर देखते हैं दैवी कार्य पूर्ण करने के लिए लौट पड़ते हैं- वह कार्य है नवीन मानवता का सृजन। यही ‘सावित्री’ की सबसे बड़ी विशेषता है।
सावित्री महाकाव्य के सम्बन्ध में कुछ लोगों को अध्यायों की संगति लगाने में कठिनाई होती है। प्रथम पर्व का प्रथम सर्ग उषःकाल के रूपक से प्रारम्भ होता है। उसमें आत्मा प्रकृति में प्रवेश करती है, जैसे अन्ध रजनी के बाद सूर्य का उदय होता है। इसमें हम सावित्री को अपने जीवन की मुख्य समस्या का सामना करते हुए देखते हैं। सत्यवान की अचानक मृत्यु से वह स्तम्भित है। उसके सामने पृथ्वी, प्रेम और काल खड़ा हुआ है। उसके हृदय में यम का सामना करने के लिए विश्वव्यापी दुःख उदय होकर उसकी शान्ति और शक्ति की परीक्षा लेता है। दूसरे पर्व में सावित्री के हृदय की आन्तरिक प्रक्रिया बतलायी गई है। विशेष अध्यायों में कवि हमें सावित्री के जन्म के पूर्व अश्वपति के राज्य में ले जाता है, उनमें हमें अश्वपति के आन्तरिक जीवन के संघर्ष और सिद्ध के दर्शन मिलते हैं, जिससे सावित्री का जन्म होता है। सिद्धि के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचकर वह पृथ्वी पर उतरते हैं। उनको आदेश मिलता है कि वे मनुष्य जाति की पूर्णता के लिए प्रयत्न करें। इस प्रयत्न में उन्हें दैवी कृपा की सहायता मिलेगी जिससे मनुष्य की समस्या हल होगी। अश्वपति के इस दिव्य यात्रा के वर्णन से ही सावित्री महाकाव्य के दूसरे और तीसरे पर्व भरे हुए हैं।
इस प्रकार ‘सावित्री’ का अर्थ होगा-साविता की पुत्री अथवा दैवी सर्जक की शक्ति। ‘सावित्री’ महाकाव्य सावित्री दैवी का प्रतीक है, जो मानव रूप में अवतरित होकर मानवात्मा को अपने दैवी लक्ष्य की ओर ले जाती है। सत्यवान का अर्थ है- जिसके पास सत्य है अथवा जो सत्य पाना चाहता है। इस काव्य में सावित्री के पिता अश्वपति को जीवन-स्वामी माना गया है। वेदों में अश्व जीवनी शक्ति का द्योतक है, अतः अश्वपति का अर्थ जीवन का स्वामी ही हो सकता है। ‘सावित्री में राजा अश्वपति पृथ्वी पर अवतरित जिज्ञासु आत्मा का प्रतीक है।
सावित्री की कथा महाभारत अरण्य पर्व अ, 208 पर आधारित है। श्री अरविन्द ने वह कथा ज्यों की त्यों रक्खी है, केवल उसे प्रतीकात्मक बना दिया है, उसे जीवित प्रतीक में बदल दिया है। प्रथम पर्व के एक कोने से तीन सर्गों में कवि ने अपनी विश्व-सृजन सम्बन्धी मान्यता का वर्णन किया है। अश्वपति का चरित्र विश्व-सृजन सम्बन्धी मान्यता का वर्णन किया है। अश्वपति का चरित्र भी उसी में वर्णित है। सत्यवान के लिए अश्वपति की तपस्या को कवि ने आत्मज्ञान और विश्वज्ञान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासु मानवता की खोज के रूप में चित्रित किया गया है। द्वितीय पर्व में अश्वपति विश्व के विभिन्न स्तरों से ऊपर उठते हुए उच्चतर मानस तथा उच्च ज्ञान के स्तर तक पहुँच जाता है। उसके हदय में जिज्ञासा की अग्नि प्रज्ज्वलित है।
अश्वपति इस पृथ्वी पर सतयुग लाना चाहते हैं। मानव चेतना कितना महान ज्ञान अर्जित कर सकती है, वह कितनी गहराई और ऊँचाई तक जा सकती है, यह अश्वपति की तपस्या से प्रकट होता है। जितनी अधिक पूर्णता इस पृथ्वी पर लाना सम्भव है। उसकी प्राप्ति के लिए उसका हृदय छटपटाता है। तृतीय पर्व में अश्वपति विश्व के ऊपर प्रवेश कर अनुभव प्राप्त करता है और सृजनशक्ति के आमने-सामने पहुँच जाता है। वह आत्मा के दिव्य लोक के दर्शन करता है जहाँ सत्य शक्ति और चेतना दिव्य आनंद और समरसता एक साथ मौजूद हैं। वह इन सब तत्त्वों को पृथ्वी पर उतारना चाहता है, पृथ्वी पर दिव्य राज्य लाना चाहता है। दैवी शक्ति से उसे वरदान प्राप्त होता है कि अन्धकार व अज्ञान शक्तियों को जीतकर सत्य को मानव जगत् में उतार सके। दैवी शक्ति उसे वरदान देती है कि उसकी कृपा पृथ्वी पर अवतरित होगी।
इस प्रकार सावित्री का पृथ्वी पर जन्म होता है। सन्तान-कामना की एक सामान्य कथा को श्रीअरविन्द ने यह दिव्य रूप दिया है। अश्वपति की यात्रा अचेतन से चेतन के उच्च स्तर पर पहुँचने की यात्रा है। इसकी कठिनाई मानवात्वा द्वारा अनुभूत विघ्न-बाधाएँ हैं जो उसे सत्यवान की प्राप्ति में सामने आती हैं और उसकी सफलता मानव-जाति के द्वारा सत्य की प्राप्ति की सफलता है।
सावित्री भी केवल महाभारत की एक सामान्य राजकुमारी न रहकर दिव्य कृपा की अवतार बन जाती है। वह मानव के दुःखों और अपमानों को सहकर अन्धता और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर दिव्यलोक की प्राप्ति करती है। वह यमराज का सामना कर अपने पति सत्यवान को मृत्युपाश से छुड़ाती है। अपनी अमरता और अनन्तता के विस्तार से ही वह यह विजय प्राप्त करती है।
सावित्री का जन्म, बाल्यकाल, पति के वरण की उसकी यात्रा, सत्यवान से मिलन वापस आने पर नारद से मिलन आदि कथाएं ज्यों की त्यों रक्खी गई हैं। अन्तर इतना ही है कि श्रीअरविन्द की सावित्री अपनी मनुष्यता के साथ अपनी दिव्यता का भी एक साथ अनुभव करती है। नारद-सावित्री-संवाद में कवि ने विश्वनियन्ता का उद्देश्य तथा मानव के अदृश्य और कर्म सिद्धान्त को उच्च शिखर पर पहुँचा दिया है।
सावित्री के 4 से 6 पर्वों में दैवी माता द्वारा दिए गए वरदान की महत्ता प्रदर्शित की गई है। यम-सावित्री केवल मानव-जाति की प्रतिनिधि नहीं है। अपितु दैवी कृपा की भी अवतार है। यम कुटिलता, प्रलोभन, छल आदि को उपस्थिति करने वाले अज्ञान का प्रतिनिधि है। सारा संवाद उच्च के उच्चतर स्तर पर उठता चला जाता है। उसमें अतिमानस क्षेत्र की ज्योति और आत्मप्रेरणा की चमक बीच-बीच में कौंध जाती है।
एक छोटे-से कथानक को कितना विस्तृत और उच्च शिखर तक पहुँचाया जा सकता है, इसका प्रमाण है ‘सावित्री’ महाकाव्य। उसमें मनोवैज्ञानिक तथ्य भरे हुए हैं, जिससे मानव-विकास हो सकता है। महाकवि की यही उन्नयन कला है, जो मानवीय है। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सावित्री का प्राचीन कथानक समाप्त हो जाता है। पिता का राज्य प्राप्त कर सावित्री और सत्यवान राज्य-सुख भोगने लगते हैं। किंतु श्री अरविन्द की ‘सावित्री’ में वे दोनों मृत्यु का राज्य पार कर अन्नत दिवस के राज्य में प्रवेश करते हैं जहाँ कि सत्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, जहाँ अज्ञान और मृत्यु का कोई स्थान नहीं है। वहाँ कुछ काल ठहरकर वे दोनों पृथ्वी की ओर देखते हैं दैवी कार्य पूर्ण करने के लिए लौट पड़ते हैं- वह कार्य है नवीन मानवता का सृजन। यही ‘सावित्री’ की सबसे बड़ी विशेषता है।
सावित्री महाकाव्य के सम्बन्ध में कुछ लोगों को अध्यायों की संगति लगाने में कठिनाई होती है। प्रथम पर्व का प्रथम सर्ग उषःकाल के रूपक से प्रारम्भ होता है। उसमें आत्मा प्रकृति में प्रवेश करती है, जैसे अन्ध रजनी के बाद सूर्य का उदय होता है। इसमें हम सावित्री को अपने जीवन की मुख्य समस्या का सामना करते हुए देखते हैं। सत्यवान की अचानक मृत्यु से वह स्तम्भित है। उसके सामने पृथ्वी, प्रेम और काल खड़ा हुआ है। उसके हृदय में यम का सामना करने के लिए विश्वव्यापी दुःख उदय होकर उसकी शान्ति और शक्ति की परीक्षा लेता है। दूसरे पर्व में सावित्री के हृदय की आन्तरिक प्रक्रिया बतलायी गई है। विशेष अध्यायों में कवि हमें सावित्री के जन्म के पूर्व अश्वपति के राज्य में ले जाता है, उनमें हमें अश्वपति के आन्तरिक जीवन के संघर्ष और सिद्ध के दर्शन मिलते हैं, जिससे सावित्री का जन्म होता है। सिद्धि के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचकर वह पृथ्वी पर उतरते हैं। उनको आदेश मिलता है कि वे मनुष्य जाति की पूर्णता के लिए प्रयत्न करें। इस प्रयत्न में उन्हें दैवी कृपा की सहायता मिलेगी जिससे मनुष्य की समस्या हल होगी। अश्वपति के इस दिव्य यात्रा के वर्णन से ही सावित्री महाकाव्य के दूसरे और तीसरे पर्व भरे हुए हैं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book