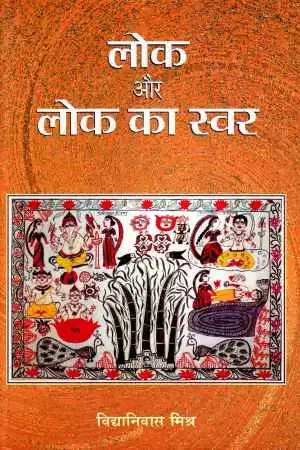|
लेख-निबंध >> लोक और लोक का स्वर लोक और लोक का स्वरविद्यानिवास मिश्र
|
16 पाठक हैं |
||||||
इसमें लोक की भारतीय जीवनसम्मत परिभाषा और उसकी अभिव्यक्ति देने का प्रयत्न किया गया है...
Lok aur lok ka swar
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
लोक-विज्ञान को ‘फोकलोरिस्टिक्स’ का तजुर्मा बना लेने के कारण लेख-संस्कृति के प्रति हमारी अवधारणा ही वह नहीं जो होनी चाहिए थी, या जो थी। हमारे यहाँ ‘लोक’ का अभिप्राय सामने वर्तमान है, दृश्यमान है, अनुभाव्यमान है। ‘फोक’ शब्द में ध्वनि व्यतीत, ग्राम्य, अर्द्धविस्मित और परिरक्षणीय की है। लोक में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए फोकलोरिस्टिक्स के संस्पर्श से लोक-वार्ता के अध्ययन में कुछ पूर्व ग्रन्थियाँ उत्पन्न हो गयी हैं और इनमें मुख्य दृष्टि परिरक्षण की है, परिवर्द्धन की नहीं। इसलिए लोक-वार्ता का अध्ययन या तो शवच्छेदन होकर रह जाता है या फिर विस्मयावेश बनकर। मैं बचपन से ही लोक के सजीव क्षेत्र में रहता हूँ। उस क्षेत्र के प्रति दया-दृष्टि मुझे बहुत चुभती है। मैंने अपने जीवन के आस-पास उसे छंदोमय गति से थिरकते पाया है।
इस पुस्तक में मैंने लोक की भारतीय जीवनसम्मत परिभाषा और उसकी अभिव्याप्ति देने का प्रयत्न किया है। उदाहरणों के चयन में कोशिश की है कि ऐसे ही उदाहरण चुने जाएँ जो भारतीय काव्य यात्रा के वाचिक पक्ष को उजागर कर सकें। इसलिए इसका नाम रखा है ‘लोक और लोक का स्वर’।
इस पुस्तक में मैंने लोक की भारतीय जीवनसम्मत परिभाषा और उसकी अभिव्याप्ति देने का प्रयत्न किया है। उदाहरणों के चयन में कोशिश की है कि ऐसे ही उदाहरण चुने जाएँ जो भारतीय काव्य यात्रा के वाचिक पक्ष को उजागर कर सकें। इसलिए इसका नाम रखा है ‘लोक और लोक का स्वर’।
अपनी बात
‘लोक और लोक का स्वर’ लिखने की आवश्यकता मुझे इसलिए प्रतीत हुई कि लोक विज्ञान को ‘फोकलोरिस्टिक्स’ का तर्जुमा बना लेने के कारण लोक संस्कृति के प्रति हमारी अवधारणा ही वह नहीं रही जो होनी चाहिए थी, या जो थी। हमारे यहाँ ‘लोक’ का अभिप्राय सामने वर्तमान है, दृश्यमान है, अनुभाव्यमान है। लोक व्यतीत नहीं है। ‘फोक’ शब्द में ध्वनि व्यतीत, ग्राम्य अर्द्धविस्मृत और परिरक्षणीय की है। लोक में ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए फोकलोरिस्टिक्स के संस्पर्श से लोक-वार्त्ता के अध्ययन में कुछ पूर्व ग्रंथियाँ उत्पन्न हो गई हैं और उनमें मुख्य दृष्टि परिरक्षण की है, परिवर्द्धन की नहीं। इसलिए लोक वार्त्ता का अध्ययन या तो शवच्छेदन होकर रह जाता है या फिर विस्मया वेश बनकर। मैं बचपन से ही लोक के सजीव क्षेत्र में रहता हूँ। उस क्षेत्र के प्रति दया दृष्टि मुझे बहुत चुभती है। मैंने अपने जीवन के आसपास उसे छंदोमय गति से थिरकते पाया है।
इस पुस्तक में मैंने लोक की भारतीय जीवनसम्मत परिभाषा और उसकी अभिव्याप्ति देने का प्रयत्न किया है। उदाहरणों के चयन में कोशिश की है कि ऐसे ही उदाहरण चुने जाएँ जो भारतीय काव्य-यात्रा के वाचिक पक्ष को उजागर कर सकें। इसीलिए इसका नाम रखा है ‘लोक और लोक का स्वर’।
लोक-वार्ता के अध्ययन में सहायता जितनी भीतर से मिलती है उतनी बाहर से नहीं। इसी भीतरवाले मन के पुनर्जागरण का समय आ गया है। इसमें अधिकांश निबंध तो भिन्न-भिन्न प्रकार की शंकाओं के समाधान के रूप में हैं, कुछ निबंध व्याख्यात्मक भी हैं। इन दोनों प्रकार के निबंधों के योग से यह पुस्तक बनी है और इसका लोकार्पण भी द्वितीय विश्व भोजपुरी सम्मेलन के अवसर पर हो रहा है। यह ध्यातव्य है कि यह पुस्तक प्रश्नों के उत्थापन के लिए ज्यादा है, शिष्टाचार के लिए कम।
इसकी प्रेस कॉपी तैयार करने और प्रूफ संशोधन में श्री राजीव कुमार पांडेय और प्रकाश उदय का सहयोग मिला है। उन्हें आशीर्वाद।
इस पुस्तक में मैंने लोक की भारतीय जीवनसम्मत परिभाषा और उसकी अभिव्याप्ति देने का प्रयत्न किया है। उदाहरणों के चयन में कोशिश की है कि ऐसे ही उदाहरण चुने जाएँ जो भारतीय काव्य-यात्रा के वाचिक पक्ष को उजागर कर सकें। इसीलिए इसका नाम रखा है ‘लोक और लोक का स्वर’।
लोक-वार्ता के अध्ययन में सहायता जितनी भीतर से मिलती है उतनी बाहर से नहीं। इसी भीतरवाले मन के पुनर्जागरण का समय आ गया है। इसमें अधिकांश निबंध तो भिन्न-भिन्न प्रकार की शंकाओं के समाधान के रूप में हैं, कुछ निबंध व्याख्यात्मक भी हैं। इन दोनों प्रकार के निबंधों के योग से यह पुस्तक बनी है और इसका लोकार्पण भी द्वितीय विश्व भोजपुरी सम्मेलन के अवसर पर हो रहा है। यह ध्यातव्य है कि यह पुस्तक प्रश्नों के उत्थापन के लिए ज्यादा है, शिष्टाचार के लिए कम।
इसकी प्रेस कॉपी तैयार करने और प्रूफ संशोधन में श्री राजीव कुमार पांडेय और प्रकाश उदय का सहयोग मिला है। उन्हें आशीर्वाद।
विद्यानिवास मिश्र
लोक और लोकातीत
लोक देश का ही एक आनुभविक रूप है। ‘लोक’ शब्द की व्युपत्पत्ति रुच/लुच से है, जिसका अर्थ प्रकाशित होना है और प्रकाशित करना भी है, जो सामने प्रकाशित दिख रहा है और जो प्रकाशित कर रहा है। इसके सजातीय शब्द हैं-आलोक लोचन (आँख), आलोचना (अच्छी तरह देखकर विवेचन करना), रोचन (प्रकाशमान, सुंदर, शोभन, इसीलिए प्रीतिकर, प्रीतिकर संदेश, संतानोत्पत्ति का संदेश इसी से संबद्ध फारसी का रोशन और रोशनी है), अवलोकन, प्रत्यवलोकन में रहते हुए लोक से ऊपर उठनेवाला) लोकायुत (ऐसा मत जो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता हो।) इस शब्द से संबद्ध अनेक शब्द यूरोप की भाषाओं में हैं, जिनमें यही अर्थ सूत्र की तरह व्याप्त है।
इस प्रकार लोक अपने में विशाल अर्थक्षेत्र समेटता है। जो भी दृष्टिगत संसार है अथवा जो भी इंद्रियगोचर संसार है, वह लोक है। इस लोक का अर्थ है-जो यहाँ है, जो प्रस्तुत है। लोक का विस्तृत अर्थ है-लोक में रहनेवाले मनुष्य, अन्य प्राणी और स्थावर संसार के पदार्थ ! क्योंकि ये सब भी प्रत्यक्ष अनुभव के विषय हैं। लोक के अर्थ का और विस्तार करते हैं तो लोक व्यवहार, लोक के द्वारा स्वीकृत व्यवहार या आचार लोक के इस अर्थ को ही लाक्षणिक रूप में लेते हुए हम कहते हैं तीन लोक-भूलोक (पृथ्वीलोक), भुवर्लोक (अंतरिक्ष) और स्वर्लोक (द्युलोक)। इन तीनों को त्रिलोकी कहते हैं। पृथ्वी के उस पार को हम पाताललोक या नागलोक या असुरलोक भी कहते हैं। इन सब प्रयोगों में यह अर्थ अभिव्याप्त है कि किसी सीमित और परिभाषित आकाश का नाम लोक है। यह लोक अवधारणा मात्र नहीं, यह कर्मक्षेत्र है।
अधिकतर लोग, जो यह समझते हैं कि भारतीय चिंतनधारा इहलोक की उपेक्षा करती है, केवल परलोक की बात करती है, वह बिलकुल गलत है। वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। प्रत्येक कर्मकांड में लोक दो दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। एक तो लोक में जो वस्तुएँ सुंदर हैं, मांगलिक हैं उनका उपयोग होता है। सात नदियों का जल या सात कुओं का जल, सात स्थानों की मिट्टी, सात ओषधियाँ, पाँच पेड़ों के पल्लव, धरती पर उगनेवाले कुश, गाँव के कुम्हार के बनाए दीये और बरतन, गाँव के बढ़ई के गढ़े पीठासन, गाँव के शिल्पी के द्वारा तैयार की हुई वस्तुएँ, ऋतु के फल फूल ये सब उपयोग में लाए जाते हैं। बिना उनके कोई अनुष्ठान नहीं पूरा होता। दूसरे, लोककंठ में बसे गीतों और गाथाओं, लोकाचार के क्रमों और लोक की मर्यादाओं का उतना ही महत्त्व माना जाता है जितना शास्त्र विधि का। शास्त्र से शुद्ध विधि भी लोक विरुद्ध होने पर अमान्य होती है। लोकाचार का अपना स्थान होता है। इसी प्रकार वेदमत, साधुमत और लोकमत तीनों के बीच सामंजस्य रखने से ही कोई व्यवस्था पूर्ण मानी जाती है। वेदमत मानने का अर्थ है- निरंतर मनन करने से जो ज्ञान की धारा स्पष्टतर होती जाती है उसके अनुसार अपना कर्तव्य पथ निश्चित करना। साधुमत का अर्थ है-सदाचारी व्यक्ति के आचरण में जो निरंतर दिखाई पड़ता है उसे मान्यता देना। लोकमत मानने का अभिप्राय है-लोक के द्वारा जो सर्वथा मान्य है उसे आदर देना। समग्र दृष्टि इन तीनों मतों के सामंजस्य से बनती है।
भारतीय चिंतनधारा एकांगिता कभी नहीं स्वीकार करती। वह उसी को मानती है, जो संपूर्ण हो, समग्र हो। शासन-व्यवस्था और न्याय-व्यवस्था ने भी लोक का प्रामाण्य स्वीकृत किया है। अदृश्य कर्म-विपाक के आधार पर या जन्मांतर के अधिकार के दावे के आधार पर न्यायालय निर्णय नहीं करता; जो भी साक्षी सामने आते हैं, वे दृष्ट प्रमाण देते हैं। कारण यह है कि जन्मांतर के अधिकार की बात करने से अधिकार का निर्णय कठिन हो जाएगा, लोक चलेगा नहीं। अदृश्य या लोकोत्तर की भूमिका व्यक्ति के जीवन में कम नहीं है, परंतु लोक की उपेक्षा करके नहीं।
श्रीकृष्ण जैसे अलौकिक चरित्र में भी आग्रह है कि मुझे भी लोकयात्रा पूरी करनी है। यदि मैं न करूँ तो यह लोक नष्ट हो जाए। लोक-संग्रह के पथ पर ज्ञानी-से-ज्ञानी विदेह-से-विदेह को अपने लिए नहीं लोक के लिए चलना पड़ता है। जीवन की सार्थकता इसी में है कि ‘यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः’। उससे लोक उद्विग्न न हो और वह स्वयं लोक से उद्विग्न न हो। इसलिए इसे ‘असिधाराव्रत’ कहा गया है। इसी लोक के भीतर से होकर लोकोत्तर की राह जाती है।
इस संक्षिप्त भूमिका के साथ लोक की अवधारणा के विकास क्रम की कुछ चर्चा करना चाहेंगे। ऋग्वेद में लोक को दिशा से पृथक् किया गया है। विराट् पुरुष के कानों से दिशाओं की उपत्ति हुई, उसके बाद लोक की हुई; इसका तात्पर्य यही है कि सापेक्ष देश के अनंतर लोक की उद्भावना हुई। ऋग्वेद में ही ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहाँ लोक का अर्थ है खुली जगह, आलोकमय स्थान, घेरे से उन्मोचन, खड़े होने की जगह; जैसे-1 ‘यो वो वृताभ्यो अकृणोद् लोकम्’) ऋग्वेद, 4/17/176) (जिसमें आपको घेरों से बाहर करके खुले स्थान की राहत दी।) 2. आर्दयद्वृत्रमकृणोदु लोकं’ (ऋग्वेद, 10/104/10) (इंद्र ने वृत्र (घेरे) को दूर किया और लोक अर्थात् खुलेपन की मुक्ति दी)। इसी लोक का प्रयोग यज्ञ के लिए निर्धारित स्थान के अर्थ में शतपथ ब्राह्मण में अनेक स्थानों में हुआ है-‘तस्मा एतं पुरस्ताल्लोकं करोति यद्दीक्षितो भवति’ (श.ब्रा., 6/2/2/27)। यज्ञ में दीक्षित होने के बाद अपने नए जनमे रूपांतर के लिए अलग स्थान बनाता है अर्थात् वह नए लोक में अधिष्ठित होता है। यज्ञस्थल संपूर्ण लोकों का प्रतिरूप है। इस प्रकार शास्त्र में रंगस्थल भी त्रिभुवन का प्रतिरूप माना जाता है और एक अधिक परिष्कृत और अनुभाव्य देशकाल की सृष्टि की जाती है, तभी नाट्य प्रत्येक देशकाल में हृदयस्पर्शी हो सकता है।
इस प्रकार लोक अपने में विशाल अर्थक्षेत्र समेटता है। जो भी दृष्टिगत संसार है अथवा जो भी इंद्रियगोचर संसार है, वह लोक है। इस लोक का अर्थ है-जो यहाँ है, जो प्रस्तुत है। लोक का विस्तृत अर्थ है-लोक में रहनेवाले मनुष्य, अन्य प्राणी और स्थावर संसार के पदार्थ ! क्योंकि ये सब भी प्रत्यक्ष अनुभव के विषय हैं। लोक के अर्थ का और विस्तार करते हैं तो लोक व्यवहार, लोक के द्वारा स्वीकृत व्यवहार या आचार लोक के इस अर्थ को ही लाक्षणिक रूप में लेते हुए हम कहते हैं तीन लोक-भूलोक (पृथ्वीलोक), भुवर्लोक (अंतरिक्ष) और स्वर्लोक (द्युलोक)। इन तीनों को त्रिलोकी कहते हैं। पृथ्वी के उस पार को हम पाताललोक या नागलोक या असुरलोक भी कहते हैं। इन सब प्रयोगों में यह अर्थ अभिव्याप्त है कि किसी सीमित और परिभाषित आकाश का नाम लोक है। यह लोक अवधारणा मात्र नहीं, यह कर्मक्षेत्र है।
अधिकतर लोग, जो यह समझते हैं कि भारतीय चिंतनधारा इहलोक की उपेक्षा करती है, केवल परलोक की बात करती है, वह बिलकुल गलत है। वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। प्रत्येक कर्मकांड में लोक दो दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। एक तो लोक में जो वस्तुएँ सुंदर हैं, मांगलिक हैं उनका उपयोग होता है। सात नदियों का जल या सात कुओं का जल, सात स्थानों की मिट्टी, सात ओषधियाँ, पाँच पेड़ों के पल्लव, धरती पर उगनेवाले कुश, गाँव के कुम्हार के बनाए दीये और बरतन, गाँव के बढ़ई के गढ़े पीठासन, गाँव के शिल्पी के द्वारा तैयार की हुई वस्तुएँ, ऋतु के फल फूल ये सब उपयोग में लाए जाते हैं। बिना उनके कोई अनुष्ठान नहीं पूरा होता। दूसरे, लोककंठ में बसे गीतों और गाथाओं, लोकाचार के क्रमों और लोक की मर्यादाओं का उतना ही महत्त्व माना जाता है जितना शास्त्र विधि का। शास्त्र से शुद्ध विधि भी लोक विरुद्ध होने पर अमान्य होती है। लोकाचार का अपना स्थान होता है। इसी प्रकार वेदमत, साधुमत और लोकमत तीनों के बीच सामंजस्य रखने से ही कोई व्यवस्था पूर्ण मानी जाती है। वेदमत मानने का अर्थ है- निरंतर मनन करने से जो ज्ञान की धारा स्पष्टतर होती जाती है उसके अनुसार अपना कर्तव्य पथ निश्चित करना। साधुमत का अर्थ है-सदाचारी व्यक्ति के आचरण में जो निरंतर दिखाई पड़ता है उसे मान्यता देना। लोकमत मानने का अभिप्राय है-लोक के द्वारा जो सर्वथा मान्य है उसे आदर देना। समग्र दृष्टि इन तीनों मतों के सामंजस्य से बनती है।
भारतीय चिंतनधारा एकांगिता कभी नहीं स्वीकार करती। वह उसी को मानती है, जो संपूर्ण हो, समग्र हो। शासन-व्यवस्था और न्याय-व्यवस्था ने भी लोक का प्रामाण्य स्वीकृत किया है। अदृश्य कर्म-विपाक के आधार पर या जन्मांतर के अधिकार के दावे के आधार पर न्यायालय निर्णय नहीं करता; जो भी साक्षी सामने आते हैं, वे दृष्ट प्रमाण देते हैं। कारण यह है कि जन्मांतर के अधिकार की बात करने से अधिकार का निर्णय कठिन हो जाएगा, लोक चलेगा नहीं। अदृश्य या लोकोत्तर की भूमिका व्यक्ति के जीवन में कम नहीं है, परंतु लोक की उपेक्षा करके नहीं।
श्रीकृष्ण जैसे अलौकिक चरित्र में भी आग्रह है कि मुझे भी लोकयात्रा पूरी करनी है। यदि मैं न करूँ तो यह लोक नष्ट हो जाए। लोक-संग्रह के पथ पर ज्ञानी-से-ज्ञानी विदेह-से-विदेह को अपने लिए नहीं लोक के लिए चलना पड़ता है। जीवन की सार्थकता इसी में है कि ‘यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः’। उससे लोक उद्विग्न न हो और वह स्वयं लोक से उद्विग्न न हो। इसलिए इसे ‘असिधाराव्रत’ कहा गया है। इसी लोक के भीतर से होकर लोकोत्तर की राह जाती है।
इस संक्षिप्त भूमिका के साथ लोक की अवधारणा के विकास क्रम की कुछ चर्चा करना चाहेंगे। ऋग्वेद में लोक को दिशा से पृथक् किया गया है। विराट् पुरुष के कानों से दिशाओं की उपत्ति हुई, उसके बाद लोक की हुई; इसका तात्पर्य यही है कि सापेक्ष देश के अनंतर लोक की उद्भावना हुई। ऋग्वेद में ही ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहाँ लोक का अर्थ है खुली जगह, आलोकमय स्थान, घेरे से उन्मोचन, खड़े होने की जगह; जैसे-1 ‘यो वो वृताभ्यो अकृणोद् लोकम्’) ऋग्वेद, 4/17/176) (जिसमें आपको घेरों से बाहर करके खुले स्थान की राहत दी।) 2. आर्दयद्वृत्रमकृणोदु लोकं’ (ऋग्वेद, 10/104/10) (इंद्र ने वृत्र (घेरे) को दूर किया और लोक अर्थात् खुलेपन की मुक्ति दी)। इसी लोक का प्रयोग यज्ञ के लिए निर्धारित स्थान के अर्थ में शतपथ ब्राह्मण में अनेक स्थानों में हुआ है-‘तस्मा एतं पुरस्ताल्लोकं करोति यद्दीक्षितो भवति’ (श.ब्रा., 6/2/2/27)। यज्ञ में दीक्षित होने के बाद अपने नए जनमे रूपांतर के लिए अलग स्थान बनाता है अर्थात् वह नए लोक में अधिष्ठित होता है। यज्ञस्थल संपूर्ण लोकों का प्रतिरूप है। इस प्रकार शास्त्र में रंगस्थल भी त्रिभुवन का प्रतिरूप माना जाता है और एक अधिक परिष्कृत और अनुभाव्य देशकाल की सृष्टि की जाती है, तभी नाट्य प्रत्येक देशकाल में हृदयस्पर्शी हो सकता है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book