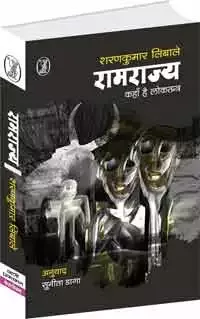|
विविध उपन्यास >> नरवानर नरवानरशरणकुमार लिंबाले
|
244 पाठक हैं |
||||||
समकालीन दलित आन्दोलन पर आधारित उपन्यास....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
1956 से 1996 तक के समय पर आधारित यह उपन्यास दरअसल आत्मचिंतन है। दलित
विमर्श के संवेदनशील विस्फोटक सन्दर्भ का एक साहित्यिक विश्लेषण। लेखक के
अनुसार इस आत्मचिन्तन के विश्लेषण के मूल में हैं कुछ स्मृतियाँ कुछ
बहसें, कुछ समाचार, कुछ साहित्यपाठ, समाज की गतिविधियाँ और उनसे उत्पन्न
प्रतिक्रियाएँ, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और व्यभिचार की उन्मुख दैनंदिनी
नैतिकता, दंगे और हिंसा, राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों को प्राप्त
प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय नेतृत्व का भ्रष्टाचार बढ़ती हुई बेरोजगारी, मँहगाई,
गरीबी और आबादी।
लेकिन मराठी में ‘उपल्या’ नाम से प्रकाशित और चर्चित इस उपन्यास की केन्द्रीय चिन्ता समकालीन दलित आन्दोलन है। पहले अध्याय में एक सनातनी ब्राह्मण परिवार के दलितीकरण का चित्रण है तो तीसरे अध्याय में एक ब्राह्मण परिवार की ही बेटी एक दलित से विवाह करके नया जीवन शुरू करती है। बाकी दो अध्यायों में दलित आन्दोलन के उभार, संघर्ष और विखंडन पर दृष्टिपात किया है। कहना न होगा कि हिन्दी और मराठी में समान रूपों से लोकप्रिय लेखक शरणकुमार लिंबाले का यह उपन्यास समकालीन दलित विमर्श के सन्दर्भ में एक जरूरी पुस्तक है।
लेकिन मराठी में ‘उपल्या’ नाम से प्रकाशित और चर्चित इस उपन्यास की केन्द्रीय चिन्ता समकालीन दलित आन्दोलन है। पहले अध्याय में एक सनातनी ब्राह्मण परिवार के दलितीकरण का चित्रण है तो तीसरे अध्याय में एक ब्राह्मण परिवार की ही बेटी एक दलित से विवाह करके नया जीवन शुरू करती है। बाकी दो अध्यायों में दलित आन्दोलन के उभार, संघर्ष और विखंडन पर दृष्टिपात किया है। कहना न होगा कि हिन्दी और मराठी में समान रूपों से लोकप्रिय लेखक शरणकुमार लिंबाले का यह उपन्यास समकालीन दलित विमर्श के सन्दर्भ में एक जरूरी पुस्तक है।
भूमिका
‘नरवानर’ एक काल्पनिक रचना है। इसमें सत्य बिलकुल ही
नहीं है।
यदि है तो सत्य का आभासमात्र है। लिखना मेरे लिए एक लत के समान है। लिखना
मेरी नितान्त व्यक्तिगत जरूरत है। मुझे जो लिखना था मैंने वह लिख दिया।
क्या सामाजिक प्रतिबद्धता किसी कलाकार की व्यक्तिगत जरूरत हो सकती है ?
डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर के महानिर्वाण के उपरान्त दलित आन्दोलन में उथल-पुथल मच गई। आन्दोलन कलह से ग्रस्त हो गया, कि बाबासाहब के निधनोपरान्त आन्दोलन की बागडोर किसके हाथ में हो। मात्र इसी विवाद ने विगत चार दशकों के इस आन्दोलन को तोड़ दिया। आन्दोलन के नेतृत्व के लिए होड़ मच गई। ‘‘असली नेता तो मैं ही हूँ। मेरा आन्दोलन ही सही आन्दोलन है’’ जैसी नारेबाजियाँ होने लगीं। कुछ लोगों ने आन्दोलन पर कब्जा करने की कोशिश की तो औरों ने अम्बेडकर के नाम पर कुछ नए आन्दोलन छेड़ दिए। आन्दोलनों की तादात बढ़ गई। सही आन्दोलन किसका है, यह देखने की अपेक्षा ‘बड़ा आन्दोलन किसका है’ यह सवाल अहम हो गया। हर एक गुट अलग-अलग अम्बेडकर जयन्ती समारोह मनाने लगा। एक चौराहे पर चार-पाँच उत्सव होने लगे। होड़ इस स्तर पर पहुँच गई कि किसकी निधि ज्यादा है। कोई आन्दोलन बिना जनसमर्थन के जीवित नहीं रह सकता। लोगों को लुभाने के लिए नई-नई तरकीबें ढूँढ़ी जाने लगीं।
लोगों की भावनाओं के समीकरण बनाए गए। जन-भावना का निरन्तर आवह्वान किया गया। रिपब्लिकन, एकता, चैत्यभूमि, दीक्षाभूमि और मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नामान्तर भावुक प्रतीक बन गए। बाबासाहब अम्बेडकर समग्र दलित चेतना के प्रतीक हैं, अतः तमाम आन्दोलन बाबासाहब अम्बेडकर का नाम लेकर ही चलने लगे। दलितों से समर्थन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने भी बाबासाहब की तस्वीर लगा दी। संघ परिवार ने भी डॉ. हेडगेवार के साथ बाबासाहब को सम्मान दिया। धीरे-धीरे बहस इस बात पर होने लगी कि असली अम्बेडकरवादी कौन है ? ‘अम्बेडकर बनाम मार्क्सवाद’, ‘अम्बेडकर बनाम गांधीवाद,’ अम्बेडकरवाद बनाम हिन्दुत्ववाद’ जैसी बहसें जोर पकड़ने लगीं। किसी को मार्क्सवादी करार देकर, किसी को समाजवादी समझकर, किसी को हिन्दुत्ववादी बताकर समाज से अलगाने की राजनीति शुरू हो गई। असली वर्गशत्रु और वर्णशत्रु नजरअंदाज हो गए। दलितों में फूट पड़ गई। आन्दोलन टूट गया, गुट बन गए।
समाज गुटों में बँट गया। इस प्रक्रिया में कुछ लोगों ने अन्य कुछ लोगों को सचमुच ही मिटा दिया। कुछ स्वयं ही अपने अनुयायियों के साथ ‘जलते घर’ (कांग्रेस) में घुस गए। वानरों की एक जाति में टोली का नर नायक अपनी टोली में पैदा होनेवाले नर बच्चों को मार डालता है। मादा पैदा होती है तो वह खुश होता है। टोली में उसके अलावा बाकी सब मादाएँ हों। भोग में कोई और भागीदार न हो। यह प्रवृत्ति उन नेताओं की थी जो सत्ता के केन्द्र में थे, अतः आन्दोलन पर एकाधिकार चाहते थे। सत्ता का भोग स्वयं करें, उसमें किसी की हिस्सेदारी न हो।
इस उपन्यास की सच्चाई की जाँच करने की अपेक्षा, मैं सोचता हूँ कि इसे एक जातक कथा के रूप में देखा जाए। पहले अध्याय में सनातनी ब्राह्मण परिवार के युवक के दलितीकरण का चित्रण है। तीसरे प्रकरण में ऐसे ही परिवार की बेटी दलित की पत्नी बनकर नया जीवन शुरू करती है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद ब्राह्मणों के दलितीकरण की प्रक्रिया का संकेत इसमें है। इन्हीं दो प्रकरणों में दलितों के ब्राह्मणीकरण की ओर भी संकेत किया गया है। व्यवस्था चाहती है कि दलित ही दलित बनकर रहे। ब्राह्मण का दलित होना या दलित का ब्राह्मण बन जाना व्यवस्था को मंजूर नहीं होता। व्यक्ति और व्यवस्था के बीच का संघर्ष इसमें महत्त्वपूर्ण बन जाता है।
दूसरे दो अध्यायों में दलित आन्दोलन का अपनी शक्ति से ऊभरना दिखाया गया है। रिपब्लिकन पार्टी, दलित पैंथर, नामान्तर आदि का परिवेश है। वर्णसत्ता और शासन के साथ दलित आन्दोलन के संघर्ष का चित्रण हुआ है। संगठन और संघर्ष ही सत्तासूत्र हैं। चौथे अध्याय में संगठन का टूटना दर्शाया गया है। आन्दोलन प्रस्थापित व्यवस्था का अंग बन जाता है। व्यवस्था मजबूत है। उसने बुद्ध, चार्वाक, महावीर और बसवेन्धर को हजम किया है। अब उसने अपने पाश बाबासाहब अम्बेडकर की दिशा में बढ़ाए हैं। दलित आन्दोलन की सन्तान है दलित साहित्य और दलित राजनीति। इनका पूरा ब्यौरा दिया गया है।
देश को आजाद हुए पचास वर्ष हो गए, फिर भी आम आदमी की रोटी का सवाल हल नहीं हुआ है। गरीब और गरीब होता जा रहा है। अमीर और अमीर। देश का विकास पंचतारांकित होटलों की छाँव में हो रहा है और आम आदमी अंजुली-भर पानी के लिए इधर-उधर भटक रहा है। आम आदमी शोषण की पूँजी बन गया है। सत्ता और आम आदमी का ऑटिड करने की एक कोशिश मैंने इस पुस्तक में की है।
यूँ तो लिखना शत-प्रतिशत यथार्थ होता नहीं। डर लगा कि अपना लिखना यथार्थवादी पूँजी तो नहीं बन जाएगा, इसलिए पात्र-प्रसंग घटनाओं का काल्पनिक होना जरूरी हो गया। पूरी कल्पना और पूरे यथार्थ का एक रसायन बनाने में काफी समय लगा। कल्पना से रचना को साकार करना कठिन होता है। कल्पना की मुट्ठी से यथार्थ छूट गया तो कल्पना में बाकी क्या रह जाएगा ? देह और प्राण का जो रिश्ता है वही किसी रचना में कल्पना और यथार्थ का होता है।
कल्पना को यथार्थ का आधार देने की कमजोर कोशिश मैंने की है। मैं सोचता हूँ कि रचना में कल्पना का अंश कितना है और यथार्थ का कितना, इस बात का हिसाब लगाना बेमानी होगा। रचना तो बस रचना होती है।
1956 से 1996 के चार दशकों के समय पर आधारित यह उपन्यास दरअसल आत्मचिन्तन है। समकालीन संवेदनशील विस्फोटक सन्दर्भ का यह साहित्यिक विश्लेषण है। इस आत्मचिन्तन या विश्लेषण के मूल में है रचनाकार का मनोराज्य। यथार्थ का साहित्यिक रूपान्तर। कुछ स्मृतियाँ, कुछ मित्रों के साथ हुई बहसें, कुछ समाचार, कुछ साहित्यपाठ, समाज की गतिविधियाँ और उनसे उत्पन्न प्रतिक्रियाएँ, बढ़ता हुआ भष्टाचार और व्यभिचार की ओर उन्मुख दैनंदिन नैतिकता, दंगे और हिंसा फिरौती के लिए दिन दहाड़े होने वाली हत्याएँ, राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों को प्राप्त प्रतिष्ठा राष्ट्रीय नेतृत्व का भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई बेरोजगारी, महँगाई, गरीबी और आबादी सब मिलकर एक रसायन बन गया जिसने मुझे यह उपन्यास लिखने के लिए उकसाया।
मराठी में ‘उपल्या’ नाम से इस उपन्यास के दो संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। श्री निशिकांत ठकार जी ने मेरी कहानियों के अनुवाद किए हैं और अब ‘नरवानर’ नाम से इस उपन्यास का भी अनुवाद किया है। उनके अनुवाद सोद्देश्य होते हैं। मराठी के दलित साहित्य और दलित आन्दोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में इनके अनुवाद सफल हो चुके हैं।
श्री राजेन्द्र यादव ने इस उपन्यास का पहला अध्याय प्रतिबद्ध पत्रिका ‘हंस’ में प्रकाशित किया था। श्रीमती रमणिका गुप्ता ने सम्पूर्ण उपन्यास को धारावाहिक रूप में प्रगतिशील पत्रिका ‘युद्धरत आम आदमी’ पत्रिका में प्रकाशित किया। दलित साहित्य में आस्था रखनेवालों का ध्यान इस उपन्यास की ओर आकर्षित हो गया।
दिल्ली दूरदर्शन के श्री रमेश शर्मा, जिन्हें मैं बड़े प्यार से ‘बाबाजी’ कहता हूँ, ने उस उपन्यास में बहुत दिलचस्पी दिखाई।
श्रीमती अर्पणा कौर के बहुमूल्य चित्र से इस उपन्यास का मुखपृष्ठ अर्थपूर्ण हो गया है।
श्री अशोक महेश्वरी अर्थात् राधाकृष्ण प्रकाशन ने इसे तुरन्त प्रकाशन के लिए स्वीकार किया।
मैं इन सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञ हूँ और इनके प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।
डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर के महानिर्वाण के उपरान्त दलित आन्दोलन में उथल-पुथल मच गई। आन्दोलन कलह से ग्रस्त हो गया, कि बाबासाहब के निधनोपरान्त आन्दोलन की बागडोर किसके हाथ में हो। मात्र इसी विवाद ने विगत चार दशकों के इस आन्दोलन को तोड़ दिया। आन्दोलन के नेतृत्व के लिए होड़ मच गई। ‘‘असली नेता तो मैं ही हूँ। मेरा आन्दोलन ही सही आन्दोलन है’’ जैसी नारेबाजियाँ होने लगीं। कुछ लोगों ने आन्दोलन पर कब्जा करने की कोशिश की तो औरों ने अम्बेडकर के नाम पर कुछ नए आन्दोलन छेड़ दिए। आन्दोलनों की तादात बढ़ गई। सही आन्दोलन किसका है, यह देखने की अपेक्षा ‘बड़ा आन्दोलन किसका है’ यह सवाल अहम हो गया। हर एक गुट अलग-अलग अम्बेडकर जयन्ती समारोह मनाने लगा। एक चौराहे पर चार-पाँच उत्सव होने लगे। होड़ इस स्तर पर पहुँच गई कि किसकी निधि ज्यादा है। कोई आन्दोलन बिना जनसमर्थन के जीवित नहीं रह सकता। लोगों को लुभाने के लिए नई-नई तरकीबें ढूँढ़ी जाने लगीं।
लोगों की भावनाओं के समीकरण बनाए गए। जन-भावना का निरन्तर आवह्वान किया गया। रिपब्लिकन, एकता, चैत्यभूमि, दीक्षाभूमि और मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नामान्तर भावुक प्रतीक बन गए। बाबासाहब अम्बेडकर समग्र दलित चेतना के प्रतीक हैं, अतः तमाम आन्दोलन बाबासाहब अम्बेडकर का नाम लेकर ही चलने लगे। दलितों से समर्थन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने भी बाबासाहब की तस्वीर लगा दी। संघ परिवार ने भी डॉ. हेडगेवार के साथ बाबासाहब को सम्मान दिया। धीरे-धीरे बहस इस बात पर होने लगी कि असली अम्बेडकरवादी कौन है ? ‘अम्बेडकर बनाम मार्क्सवाद’, ‘अम्बेडकर बनाम गांधीवाद,’ अम्बेडकरवाद बनाम हिन्दुत्ववाद’ जैसी बहसें जोर पकड़ने लगीं। किसी को मार्क्सवादी करार देकर, किसी को समाजवादी समझकर, किसी को हिन्दुत्ववादी बताकर समाज से अलगाने की राजनीति शुरू हो गई। असली वर्गशत्रु और वर्णशत्रु नजरअंदाज हो गए। दलितों में फूट पड़ गई। आन्दोलन टूट गया, गुट बन गए।
समाज गुटों में बँट गया। इस प्रक्रिया में कुछ लोगों ने अन्य कुछ लोगों को सचमुच ही मिटा दिया। कुछ स्वयं ही अपने अनुयायियों के साथ ‘जलते घर’ (कांग्रेस) में घुस गए। वानरों की एक जाति में टोली का नर नायक अपनी टोली में पैदा होनेवाले नर बच्चों को मार डालता है। मादा पैदा होती है तो वह खुश होता है। टोली में उसके अलावा बाकी सब मादाएँ हों। भोग में कोई और भागीदार न हो। यह प्रवृत्ति उन नेताओं की थी जो सत्ता के केन्द्र में थे, अतः आन्दोलन पर एकाधिकार चाहते थे। सत्ता का भोग स्वयं करें, उसमें किसी की हिस्सेदारी न हो।
इस उपन्यास की सच्चाई की जाँच करने की अपेक्षा, मैं सोचता हूँ कि इसे एक जातक कथा के रूप में देखा जाए। पहले अध्याय में सनातनी ब्राह्मण परिवार के युवक के दलितीकरण का चित्रण है। तीसरे प्रकरण में ऐसे ही परिवार की बेटी दलित की पत्नी बनकर नया जीवन शुरू करती है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद ब्राह्मणों के दलितीकरण की प्रक्रिया का संकेत इसमें है। इन्हीं दो प्रकरणों में दलितों के ब्राह्मणीकरण की ओर भी संकेत किया गया है। व्यवस्था चाहती है कि दलित ही दलित बनकर रहे। ब्राह्मण का दलित होना या दलित का ब्राह्मण बन जाना व्यवस्था को मंजूर नहीं होता। व्यक्ति और व्यवस्था के बीच का संघर्ष इसमें महत्त्वपूर्ण बन जाता है।
दूसरे दो अध्यायों में दलित आन्दोलन का अपनी शक्ति से ऊभरना दिखाया गया है। रिपब्लिकन पार्टी, दलित पैंथर, नामान्तर आदि का परिवेश है। वर्णसत्ता और शासन के साथ दलित आन्दोलन के संघर्ष का चित्रण हुआ है। संगठन और संघर्ष ही सत्तासूत्र हैं। चौथे अध्याय में संगठन का टूटना दर्शाया गया है। आन्दोलन प्रस्थापित व्यवस्था का अंग बन जाता है। व्यवस्था मजबूत है। उसने बुद्ध, चार्वाक, महावीर और बसवेन्धर को हजम किया है। अब उसने अपने पाश बाबासाहब अम्बेडकर की दिशा में बढ़ाए हैं। दलित आन्दोलन की सन्तान है दलित साहित्य और दलित राजनीति। इनका पूरा ब्यौरा दिया गया है।
देश को आजाद हुए पचास वर्ष हो गए, फिर भी आम आदमी की रोटी का सवाल हल नहीं हुआ है। गरीब और गरीब होता जा रहा है। अमीर और अमीर। देश का विकास पंचतारांकित होटलों की छाँव में हो रहा है और आम आदमी अंजुली-भर पानी के लिए इधर-उधर भटक रहा है। आम आदमी शोषण की पूँजी बन गया है। सत्ता और आम आदमी का ऑटिड करने की एक कोशिश मैंने इस पुस्तक में की है।
यूँ तो लिखना शत-प्रतिशत यथार्थ होता नहीं। डर लगा कि अपना लिखना यथार्थवादी पूँजी तो नहीं बन जाएगा, इसलिए पात्र-प्रसंग घटनाओं का काल्पनिक होना जरूरी हो गया। पूरी कल्पना और पूरे यथार्थ का एक रसायन बनाने में काफी समय लगा। कल्पना से रचना को साकार करना कठिन होता है। कल्पना की मुट्ठी से यथार्थ छूट गया तो कल्पना में बाकी क्या रह जाएगा ? देह और प्राण का जो रिश्ता है वही किसी रचना में कल्पना और यथार्थ का होता है।
कल्पना को यथार्थ का आधार देने की कमजोर कोशिश मैंने की है। मैं सोचता हूँ कि रचना में कल्पना का अंश कितना है और यथार्थ का कितना, इस बात का हिसाब लगाना बेमानी होगा। रचना तो बस रचना होती है।
1956 से 1996 के चार दशकों के समय पर आधारित यह उपन्यास दरअसल आत्मचिन्तन है। समकालीन संवेदनशील विस्फोटक सन्दर्भ का यह साहित्यिक विश्लेषण है। इस आत्मचिन्तन या विश्लेषण के मूल में है रचनाकार का मनोराज्य। यथार्थ का साहित्यिक रूपान्तर। कुछ स्मृतियाँ, कुछ मित्रों के साथ हुई बहसें, कुछ समाचार, कुछ साहित्यपाठ, समाज की गतिविधियाँ और उनसे उत्पन्न प्रतिक्रियाएँ, बढ़ता हुआ भष्टाचार और व्यभिचार की ओर उन्मुख दैनंदिन नैतिकता, दंगे और हिंसा फिरौती के लिए दिन दहाड़े होने वाली हत्याएँ, राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों को प्राप्त प्रतिष्ठा राष्ट्रीय नेतृत्व का भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई बेरोजगारी, महँगाई, गरीबी और आबादी सब मिलकर एक रसायन बन गया जिसने मुझे यह उपन्यास लिखने के लिए उकसाया।
मराठी में ‘उपल्या’ नाम से इस उपन्यास के दो संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। श्री निशिकांत ठकार जी ने मेरी कहानियों के अनुवाद किए हैं और अब ‘नरवानर’ नाम से इस उपन्यास का भी अनुवाद किया है। उनके अनुवाद सोद्देश्य होते हैं। मराठी के दलित साहित्य और दलित आन्दोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में इनके अनुवाद सफल हो चुके हैं।
श्री राजेन्द्र यादव ने इस उपन्यास का पहला अध्याय प्रतिबद्ध पत्रिका ‘हंस’ में प्रकाशित किया था। श्रीमती रमणिका गुप्ता ने सम्पूर्ण उपन्यास को धारावाहिक रूप में प्रगतिशील पत्रिका ‘युद्धरत आम आदमी’ पत्रिका में प्रकाशित किया। दलित साहित्य में आस्था रखनेवालों का ध्यान इस उपन्यास की ओर आकर्षित हो गया।
दिल्ली दूरदर्शन के श्री रमेश शर्मा, जिन्हें मैं बड़े प्यार से ‘बाबाजी’ कहता हूँ, ने उस उपन्यास में बहुत दिलचस्पी दिखाई।
श्रीमती अर्पणा कौर के बहुमूल्य चित्र से इस उपन्यास का मुखपृष्ठ अर्थपूर्ण हो गया है।
श्री अशोक महेश्वरी अर्थात् राधाकृष्ण प्रकाशन ने इसे तुरन्त प्रकाशन के लिए स्वीकार किया।
मैं इन सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञ हूँ और इनके प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।
शरणकुमार लिब्बाले
नरवानर
मैंने दरवाजा खोल दिया, ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने रंडीबाज पति
के लिए खोलती है। मिलिन्द और रोहिदास अन्दर चले आए। उनके चेहरे बता रहे थे
कि कोई भयानक घटना घटी है, फिर भी उनका व्यवहार हस्बेमामूल था। मैं नख से
शिख तक जल उठा।
रोहिदास के कारण मिलिन्द के साथ मेरा दो बार जोर का झगड़ा हो चुका था। मैंने रेक्टर के पास शिकायत भी की थी लेकिन कुछ हुआ नहीं।
रोहिदास मिलिन्द का दोस्त था और मिलिन्द मेरा रूम पार्टनर। मेरा और मिलिन्द का अंकों का प्रतिशत सत्तर से अधिक था इसलिए हमें एक ही कमरा मिला था। रोहिदास हमारे कमरे पर गेस्ट बनकर रहता था। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं पार्टनर बदलने में कामयाब नहीं हुआ।
अछूत का रूम पार्टनर होना सजा ही तो थी। धर्म के अनुसार ब्राह्मण और अछूत को साथ रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं रहता हूँ। शायद इसी को जनतन्त्र कहते होंगे।
मैं नख से शिख तक उबल पड़ा।
बाघ, शेर, हाथी, शियार, खरगोश, कुत्ता, गधा, घोड़ा और सुअर-इन सबको एक बाड़े में बन्द करके कह दो कि तुम सब आजाद हो, सब समान हो, एक दूसरे के भाई हो-शायद ऐसे अभयारण्य को ही राष्ट्र कहते होंगे।
हिन्दू-हिन्दू, बन्धु-बन्धु।
धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण और शूद्र बन्धु नहीं हो सकते। फिर भी यह वंचना क्यों ?
मेरे विशुद्ध हिन्दुत्व को यहाँ क्यों नकारा जा रहा है ?
मैं मोमबत्ती की तरह बूँद-बूँद पिघलता जा रहा हूँ।
मैंने अपनी दीवार पर प्रभु रामचन्द्र का कैलेंडर लगाया तो मिलिन्द ने अपनी तरफ की दीवार पर अम्बेडकर की तस्वीर लटका दी। कई बार मेरे मन में आया कि इस तस्वीर को फाड़कर बाहर फेंक दूँ।
‘‘गोमांस खाओगे ?’’ मिलन्द ने पूछा।
‘‘मेरा भोजन हो चुका है।’’ मेरा स्पष्ट और कड़वाहट भरा जवाब था।
मिलिन्द की यह आदत बन चुकी है। पहली बार जब उसने पूछा था कि गोमांस खाओगे ? तब मैंने बहुत झगड़ा किया था-‘‘मैं गाय को पवित्र मानता हूँ। गो-माता का मांस खाने का मतलब है अपनी माँ का मांस खाना। तुम लोग अभक्ष्य भक्षण करते हो इसीलिए तुम्हारी यह हालत हो गई है।’’
मेरे गुस्से पर मिलिन्द बेशर्मी से हँस पड़ा था।
‘‘अरे, अपने पूर्वजों ने गोमांस खाया है, सोमरस पिया है। इतिहास पढ़ो। तुम लोगों ने गोमांस खाना छोड़ दिया और तुम सवर्ण बन गए। हम गोमांस खाते रहे और अछूत हो गए।’’
मैंने झट से कहा-‘‘तो फिर तुम भी अभक्ष्य भक्षण करना बन्द कर दो।’’
मिलिन्द उछलकर कुछ कहने ही वाला था लेकिन गले में कौर अटक जाने से छटपटाकर रह गया। उसने पानी पिया। लम्बी साँस भरकर वह कुछ कहने ही वाला था कि मैंने उसे रोक लिया-
‘‘पहले भोजन कर लो, बाद में बातें करेंगे।’’-तो उसने थाली दूर हटा दी।
‘‘पहले मुझे बोलने दो। मैं भूखा रह गया तो भी चलेगा। मेरे लिए खाना कोई अहमियत नहीं रखता...’’-और मिलिन्द बोलने लगा। वह अंगारे की तरह धधक रहा था।
‘‘मुसलमान गोमांस खाते हैं। क्या उन्हें अछूत माना जाता है ?’’ ईसाई गोमांस खाते हैं। क्या उन्हें अछूत माना जाता है ? फिर हम ही कैसे अछूत हुए ?’’
मैं मिलिन्द के सवाल का जवाब नहीं दे सका था। तब से मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया। जब भी मिलिन्द पूछता-गोमांस खाओगे ?’’ मैं शान्ति से इनकार कर देता हूँ।
‘‘अरे, थोड़ा-सा खा लो। बहुत अच्छा लगता है। देखो तो खाके, दे दूँ ? गोमांस खाने से आदमी मर नहीं जाता, बलवान हो जाता है। खाओगे ?’’
मिलिन्द जान-बूझकर मुझे छेड़ रहा था। इस स्वराज में हमारे ब्राह्मणत्व को इसी तरह मारा जाएगा। मिलिन्द भोजन करने के बाद अंगड़ाइयाँ लेता है। मन-ही-मन मैंने सोचा अगले जन्म में यह गधा बनेगा।
मुझे वह दिन याद आता है जब रोहिदास पहली बार कमरे में आया था। तभी से मेरे मन में उसके प्रति किसी डबरे की तरह नफरत और घिन जमा हो गई। उसका अनुशासनहीन बर्ताव मेरे सन्ताप का कारण बना। एक बार उसने बिना पूछे मेरा टूथपेस्ट ले लिया था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे साफ-साफ बता दिया कि बिना मेरी इजाजत के मेरी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। लेकिन फिर एक बार रोहिदास ने मेरा तौलिया इस्तेमाल किया। मैं रूम में नहीं था यह देखकर उसने मेरा तौलिया ले लिया था। जब वह उससे हाथ-मुँह पोंछ ही रहा था कि मैं कमरे में दाखिल हुआ और हमारा झगड़ा शुरू हो गया।
‘‘तुम दूसरे का तौलिया क्यों इस्तेमाल करते हो ?’’ मैं जोर से चिल्लाया।
‘‘यह जाति ही नीच है। गन्दी। साफ रहो तो स्पृश्य बनोगे ना। अस्वच्छता ही दरअसल अस्पृश्यता है।’’
मिलिन्द ने दम भरके कहा-‘‘सूट-बूट पहननेवाले दलित को भी कोई ब्राह्मण नहीं कहेंगे। अस्पृश्यता तो लोगों के मन में बसी हुई है। मुझे तो हर सवर्ण सिरफिरा लगता है।’’
रोहिदास ने मिलिन्द को शान्त किया।
लेकिन मैं धुँधुआ रहा था।
‘‘अरे, मैं तो तुम लोगों को अच्छी बात बता रहा हूँ..लेकिन तुम्हारा एप्रोच तो एकदम निगेटिव है। हर बात में आक्रामक और कट्टर ! तुम खतरनाक बात कर रहे हो...।’’
मैं कुछ शान्त होने लगा तो रोहिदास ने जबान खोली-
‘‘भला क्या है, बुरा क्या है यह तय करने का और हमें बताने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है ?’’
मैं उलझन में पड़ गया। उसके सवाल ने मुझे झकझोर डाला। यह कहना तो ठीक है कि मेरा तौलिया मत लो, लेकिन उन्हें साफ-सुथरा रहने के लिए कहना कुछ ज्यादती ही थी।
रोहिदास, मिलिन्द और मुझसे सीनियर था। वह दलित छात्र-संगठन का काम करता था और इसी कारण स्नातक परीक्षा में फेल हो गया था। वह इसी कॉलेज का पुराना छात्र था। रेक्टर से लेकर प्राचार्य तक सब से उसकी पहचान थी। कॉलेज छूट गया, फिर भी होस्टल नहीं छोड़ता। हमेशा गेस्ट बनकर रहता।
मिलिन्द और रोहिदास ने रूम का सारा फर्नीचर अपने कब्जे में कर लिया था। रूम को कार्यालय बनाया गया। रूम में हमेशा संगठन की चर्चाएँ हुआ करतीं। मैं अलग-थलग पड़ गया था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि इस रूम में गेस्ट मैं ही हूँ। मुझे बेहद गुस्सा आता था लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। मेरी यह राय कायम होती गई कि सिर्फ झुँझलाते रहना नपुंसक व्यक्ति का लक्षण है।
कल मिलिन्द से मेरा जोरदार झगड़ा हो गया। उसका कारण भी रोहिदास ही था।
सन्ध्या का समय था। मैं पढ़ रहा था। रोहिदास ने मेरा टेप ऑन कर दिया। इससे मैं भड़क उठा-
‘‘रोहिदास, तुम कितने दिन यहाँ रहनेवाले हो ? रूम में गेस्ट अलाऊड नहीं है, फिर तुम यहाँ कैसे रहते हो ?’’
‘‘हर रूम में गेस्ट हैं। गेस्ट को रखना है या नहीं, इसे रेक्टर देख लेगा। तुम्हें क्या तकलीफ है ?’’
‘‘मेरी प्राईवेसी डिस्टर्ब होती है। मुझे यहाँ भीड़ नहीं चाहिए। मेरी पढ़ाई पर असर पड़ता है।’’
‘‘हमने तुम्हें पढ़ने से कब मना किया ?’’
‘‘मुझे मेरे रूम में गेस्ट नहीं चाहिए।’’
‘‘कल तुम्हारा भी गेस्ट आ सकता है। तब....?’’
‘‘मेरा गेस्ट नहीं आएगा। आया भी तो हमेशा के लिए नहीं आएगा।’’
‘‘मेरा गेस्ट यहाँ हमेशा के लिए रहेगा। तुम्हें जो कुछ करना है, कर लो....’’ मिलिन्द ने कहा।
‘‘मै इस पंखे से लटककर फाँसी लगा लूँगा। तुम लोग मुझे मानसिक यन्त्रणा दे रहे हो।’’ मेरा गुस्सा बेकाबू हो चला था। मेरी आवाज जैसे मेरे पूरे बदन से फूट रही थी। आँखों में तड़प थी। स्थिति को भाँपकर रोहिदास चुपचाप बाहर चला गया।
मुझे खुशी हुई कि मैं जीत गया। लेकिन मिलिन्द बहुत परेशान हो गया। श्मशान की ओर जा रही अन्तिम यात्रा का-सा भाव उसके चेहरे पर था।
मैं फ्रेश हो गया। टेप लगा दिया। भीमसेन जोशी के भक्ति गीत पूरे कमरे में गूँजने लगे।
इस पर मिलिन्द उबल पड़ा-
‘‘टेप बन्द करो। मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ।’’
मैंने उलटकर कहा-
‘‘संगीत से कोई डिस्टर्ब नहीं होता।’’
‘‘टेप बन्द करो, वर्ना मैं इसे उठाकर बाहर फेंक दूँगा। मुझे शान्ति चाहिए।’’ मैंने टेप बन्द कर दिया। यह शव के सामने पूजा-पाठ करने जैसी बात थी।’’ बाजू के कमरे में अन्त्याक्षरी चल रही थी। भीड़ के गाए गाने, खिड़की पर इस तरह टकरा रहे थे जैसे भारी पथराव हो रहा हो। मैंने मिलिन्द को बोलने के लिए विवश किया-
‘‘तुम्हें गाने से परेशानी होती है ना, तो फिर जाओ, करो अन्त्याक्षरी बन्द।’’
‘‘बाहर क्या हो रहा है। इससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है।’’
‘‘मिलिन्द, हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं। रोहितास फेल हो गया है। तुम उसकी संगत में मत पड़ो, तुम भी फेल हो जाओगे। सरकार ने तुम लोगों को सहूलियतें दी हैं, उनका फायदा उठाओ।’’
‘‘सरकार हम पर कोई अहसान नहीं कर रही है।’’
‘‘लेकिन...’’
‘‘मुझे तुम्हारा उपेदश नहीं चाहिए, प्लीज।’’
‘‘मिलिन्द सुनने की मनोदशा में नहीं था। मैं उसे काँटे की तरह चुभ रहा था। मैं उसके भले की ही बात कह रहा था लेकिन वह माने तब न ! मैं चाहता था कि मेरे कमरे में पढ़ाई की चर्चाएँ हों लेकिन यहाँ रात-दिन संगठन की बातें होती थीं। मुझे यह नहीं चाहिए था। हम पढ़ाई करने आए हैं, हमें बस पढ़ाई ही करनी चाहिए।
मिलिन्द ने सिगरेट सुलगाई। धुएँ की लहरें उठने लगीं। मुझे गुस्सा आ गया। जोर से चिल्लाने को जी हुआ ‘नो स्मोकिंग !’’ लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया। ज्यादा तानना भी ठीक नहीं। वह समझ गया कि मैं नाराज हो गया हूँ।
रोहिदास रूम से चला गया यह तो अच्छा ही हुआ। कभी-न-कभी यह होना ही था। आज ही हो गया।
मेरी नस-नस में द्वेष और विद्रोह की लहरें भड़कने लगी थीं-
‘मस्ती आ गई है। सरकार इन्हें सहूलियतें दे रही है और ये हैं कि बीड़ियाँ पी रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, मुफ्त के वजीफे लेते हैं। होस्टल में कचरा भरा हुआ है। थर्ड क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्हें आसानी से प्रवेश मिल जाता है और हम बुद्धिमान हैं, फिर भी प्रवेश नहीं। हम सवर्ण हैं, इसमें हमारा क्या दोष है ? जो गद्दी पर बैठते रहे हैं अब जूते के पास बैठे हैं और जो जूते के पास थे सिंहासन पर बैठे हैं। अच्छा होता यदि हम भी चमार होते ! सहूलियतें मिल जातीं। सरकार कमअक्ल लोगों को बढ़ावा दे रही है। सरकार ऐसे लोगों पर पैसा क्यों बरबाद करे ? दलित मतों के लिए सरकार इन्हें खुश कर रही है। मुझे लगता है कि इन सब अछूतों को इकट्ठा करके उन पर एक बम गिरा देना चाहिए।’
‘‘गुस्से में तुम कहीं सचमुच तो फाँसी नहीं लगा लोगे, इसी चिन्ता में मैं रात-भर नहीं सोया।’’ रोहिदास की बात में कड़वाहट नहीं थी
‘‘मैंने रात में कई बार उठकर देखा। यह तो आराम से खर्राटे भर रहा था।’’ मिलिन्द ने मजाक में कहा।
मुझसे भी रहा नहीं गया।
‘‘रात कहाँ सोए थे ?’’
‘‘गौतम गांगुर्डे के कमरे में। मैंने तो बस स्टैंड पर भी ऐसी कई रातें गुजारी हैं।’’ महार-चमारों में यह अच्छा है, कैसे भी जी लेते हैं !
मिलिन्द और रोहिदास सोने की तैयारी करने लगे। मैंने टोका-
‘‘लगता है, आज यहीं सोओगे ?’’
रोहिदास, ने सिर हिलाया-
‘‘कल से गांगुर्डे के कमरे में रहूंगा। आज उसके पास कुछ गेस्ट आए हैं, इसलिए वहाँ जगह नहीं है।’’
मैंने कुछ नहीं कहा। इस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए हम दोनों को चुप ही रहना चाहिए।
आँख कब लग गई, पता नहीं चला। कानाफूसी की आवाज से नींद उचटी। मिलिन्द और रोहिदास के बीच बातचीत हो रही थी। उनकी बातों से घटना का पता चल रहा था।
रोहिदास के कारण मिलिन्द के साथ मेरा दो बार जोर का झगड़ा हो चुका था। मैंने रेक्टर के पास शिकायत भी की थी लेकिन कुछ हुआ नहीं।
रोहिदास मिलिन्द का दोस्त था और मिलिन्द मेरा रूम पार्टनर। मेरा और मिलिन्द का अंकों का प्रतिशत सत्तर से अधिक था इसलिए हमें एक ही कमरा मिला था। रोहिदास हमारे कमरे पर गेस्ट बनकर रहता था। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं पार्टनर बदलने में कामयाब नहीं हुआ।
अछूत का रूम पार्टनर होना सजा ही तो थी। धर्म के अनुसार ब्राह्मण और अछूत को साथ रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं रहता हूँ। शायद इसी को जनतन्त्र कहते होंगे।
मैं नख से शिख तक उबल पड़ा।
बाघ, शेर, हाथी, शियार, खरगोश, कुत्ता, गधा, घोड़ा और सुअर-इन सबको एक बाड़े में बन्द करके कह दो कि तुम सब आजाद हो, सब समान हो, एक दूसरे के भाई हो-शायद ऐसे अभयारण्य को ही राष्ट्र कहते होंगे।
हिन्दू-हिन्दू, बन्धु-बन्धु।
धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण और शूद्र बन्धु नहीं हो सकते। फिर भी यह वंचना क्यों ?
मेरे विशुद्ध हिन्दुत्व को यहाँ क्यों नकारा जा रहा है ?
मैं मोमबत्ती की तरह बूँद-बूँद पिघलता जा रहा हूँ।
मैंने अपनी दीवार पर प्रभु रामचन्द्र का कैलेंडर लगाया तो मिलिन्द ने अपनी तरफ की दीवार पर अम्बेडकर की तस्वीर लटका दी। कई बार मेरे मन में आया कि इस तस्वीर को फाड़कर बाहर फेंक दूँ।
‘‘गोमांस खाओगे ?’’ मिलन्द ने पूछा।
‘‘मेरा भोजन हो चुका है।’’ मेरा स्पष्ट और कड़वाहट भरा जवाब था।
मिलिन्द की यह आदत बन चुकी है। पहली बार जब उसने पूछा था कि गोमांस खाओगे ? तब मैंने बहुत झगड़ा किया था-‘‘मैं गाय को पवित्र मानता हूँ। गो-माता का मांस खाने का मतलब है अपनी माँ का मांस खाना। तुम लोग अभक्ष्य भक्षण करते हो इसीलिए तुम्हारी यह हालत हो गई है।’’
मेरे गुस्से पर मिलिन्द बेशर्मी से हँस पड़ा था।
‘‘अरे, अपने पूर्वजों ने गोमांस खाया है, सोमरस पिया है। इतिहास पढ़ो। तुम लोगों ने गोमांस खाना छोड़ दिया और तुम सवर्ण बन गए। हम गोमांस खाते रहे और अछूत हो गए।’’
मैंने झट से कहा-‘‘तो फिर तुम भी अभक्ष्य भक्षण करना बन्द कर दो।’’
मिलिन्द उछलकर कुछ कहने ही वाला था लेकिन गले में कौर अटक जाने से छटपटाकर रह गया। उसने पानी पिया। लम्बी साँस भरकर वह कुछ कहने ही वाला था कि मैंने उसे रोक लिया-
‘‘पहले भोजन कर लो, बाद में बातें करेंगे।’’-तो उसने थाली दूर हटा दी।
‘‘पहले मुझे बोलने दो। मैं भूखा रह गया तो भी चलेगा। मेरे लिए खाना कोई अहमियत नहीं रखता...’’-और मिलिन्द बोलने लगा। वह अंगारे की तरह धधक रहा था।
‘‘मुसलमान गोमांस खाते हैं। क्या उन्हें अछूत माना जाता है ?’’ ईसाई गोमांस खाते हैं। क्या उन्हें अछूत माना जाता है ? फिर हम ही कैसे अछूत हुए ?’’
मैं मिलिन्द के सवाल का जवाब नहीं दे सका था। तब से मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया। जब भी मिलिन्द पूछता-गोमांस खाओगे ?’’ मैं शान्ति से इनकार कर देता हूँ।
‘‘अरे, थोड़ा-सा खा लो। बहुत अच्छा लगता है। देखो तो खाके, दे दूँ ? गोमांस खाने से आदमी मर नहीं जाता, बलवान हो जाता है। खाओगे ?’’
मिलिन्द जान-बूझकर मुझे छेड़ रहा था। इस स्वराज में हमारे ब्राह्मणत्व को इसी तरह मारा जाएगा। मिलिन्द भोजन करने के बाद अंगड़ाइयाँ लेता है। मन-ही-मन मैंने सोचा अगले जन्म में यह गधा बनेगा।
मुझे वह दिन याद आता है जब रोहिदास पहली बार कमरे में आया था। तभी से मेरे मन में उसके प्रति किसी डबरे की तरह नफरत और घिन जमा हो गई। उसका अनुशासनहीन बर्ताव मेरे सन्ताप का कारण बना। एक बार उसने बिना पूछे मेरा टूथपेस्ट ले लिया था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे साफ-साफ बता दिया कि बिना मेरी इजाजत के मेरी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। लेकिन फिर एक बार रोहिदास ने मेरा तौलिया इस्तेमाल किया। मैं रूम में नहीं था यह देखकर उसने मेरा तौलिया ले लिया था। जब वह उससे हाथ-मुँह पोंछ ही रहा था कि मैं कमरे में दाखिल हुआ और हमारा झगड़ा शुरू हो गया।
‘‘तुम दूसरे का तौलिया क्यों इस्तेमाल करते हो ?’’ मैं जोर से चिल्लाया।
‘‘यह जाति ही नीच है। गन्दी। साफ रहो तो स्पृश्य बनोगे ना। अस्वच्छता ही दरअसल अस्पृश्यता है।’’
मिलिन्द ने दम भरके कहा-‘‘सूट-बूट पहननेवाले दलित को भी कोई ब्राह्मण नहीं कहेंगे। अस्पृश्यता तो लोगों के मन में बसी हुई है। मुझे तो हर सवर्ण सिरफिरा लगता है।’’
रोहिदास ने मिलिन्द को शान्त किया।
लेकिन मैं धुँधुआ रहा था।
‘‘अरे, मैं तो तुम लोगों को अच्छी बात बता रहा हूँ..लेकिन तुम्हारा एप्रोच तो एकदम निगेटिव है। हर बात में आक्रामक और कट्टर ! तुम खतरनाक बात कर रहे हो...।’’
मैं कुछ शान्त होने लगा तो रोहिदास ने जबान खोली-
‘‘भला क्या है, बुरा क्या है यह तय करने का और हमें बताने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है ?’’
मैं उलझन में पड़ गया। उसके सवाल ने मुझे झकझोर डाला। यह कहना तो ठीक है कि मेरा तौलिया मत लो, लेकिन उन्हें साफ-सुथरा रहने के लिए कहना कुछ ज्यादती ही थी।
रोहिदास, मिलिन्द और मुझसे सीनियर था। वह दलित छात्र-संगठन का काम करता था और इसी कारण स्नातक परीक्षा में फेल हो गया था। वह इसी कॉलेज का पुराना छात्र था। रेक्टर से लेकर प्राचार्य तक सब से उसकी पहचान थी। कॉलेज छूट गया, फिर भी होस्टल नहीं छोड़ता। हमेशा गेस्ट बनकर रहता।
मिलिन्द और रोहिदास ने रूम का सारा फर्नीचर अपने कब्जे में कर लिया था। रूम को कार्यालय बनाया गया। रूम में हमेशा संगठन की चर्चाएँ हुआ करतीं। मैं अलग-थलग पड़ गया था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि इस रूम में गेस्ट मैं ही हूँ। मुझे बेहद गुस्सा आता था लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। मेरी यह राय कायम होती गई कि सिर्फ झुँझलाते रहना नपुंसक व्यक्ति का लक्षण है।
कल मिलिन्द से मेरा जोरदार झगड़ा हो गया। उसका कारण भी रोहिदास ही था।
सन्ध्या का समय था। मैं पढ़ रहा था। रोहिदास ने मेरा टेप ऑन कर दिया। इससे मैं भड़क उठा-
‘‘रोहिदास, तुम कितने दिन यहाँ रहनेवाले हो ? रूम में गेस्ट अलाऊड नहीं है, फिर तुम यहाँ कैसे रहते हो ?’’
‘‘हर रूम में गेस्ट हैं। गेस्ट को रखना है या नहीं, इसे रेक्टर देख लेगा। तुम्हें क्या तकलीफ है ?’’
‘‘मेरी प्राईवेसी डिस्टर्ब होती है। मुझे यहाँ भीड़ नहीं चाहिए। मेरी पढ़ाई पर असर पड़ता है।’’
‘‘हमने तुम्हें पढ़ने से कब मना किया ?’’
‘‘मुझे मेरे रूम में गेस्ट नहीं चाहिए।’’
‘‘कल तुम्हारा भी गेस्ट आ सकता है। तब....?’’
‘‘मेरा गेस्ट नहीं आएगा। आया भी तो हमेशा के लिए नहीं आएगा।’’
‘‘मेरा गेस्ट यहाँ हमेशा के लिए रहेगा। तुम्हें जो कुछ करना है, कर लो....’’ मिलिन्द ने कहा।
‘‘मै इस पंखे से लटककर फाँसी लगा लूँगा। तुम लोग मुझे मानसिक यन्त्रणा दे रहे हो।’’ मेरा गुस्सा बेकाबू हो चला था। मेरी आवाज जैसे मेरे पूरे बदन से फूट रही थी। आँखों में तड़प थी। स्थिति को भाँपकर रोहिदास चुपचाप बाहर चला गया।
मुझे खुशी हुई कि मैं जीत गया। लेकिन मिलिन्द बहुत परेशान हो गया। श्मशान की ओर जा रही अन्तिम यात्रा का-सा भाव उसके चेहरे पर था।
मैं फ्रेश हो गया। टेप लगा दिया। भीमसेन जोशी के भक्ति गीत पूरे कमरे में गूँजने लगे।
इस पर मिलिन्द उबल पड़ा-
‘‘टेप बन्द करो। मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ।’’
मैंने उलटकर कहा-
‘‘संगीत से कोई डिस्टर्ब नहीं होता।’’
‘‘टेप बन्द करो, वर्ना मैं इसे उठाकर बाहर फेंक दूँगा। मुझे शान्ति चाहिए।’’ मैंने टेप बन्द कर दिया। यह शव के सामने पूजा-पाठ करने जैसी बात थी।’’ बाजू के कमरे में अन्त्याक्षरी चल रही थी। भीड़ के गाए गाने, खिड़की पर इस तरह टकरा रहे थे जैसे भारी पथराव हो रहा हो। मैंने मिलिन्द को बोलने के लिए विवश किया-
‘‘तुम्हें गाने से परेशानी होती है ना, तो फिर जाओ, करो अन्त्याक्षरी बन्द।’’
‘‘बाहर क्या हो रहा है। इससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है।’’
‘‘मिलिन्द, हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं। रोहितास फेल हो गया है। तुम उसकी संगत में मत पड़ो, तुम भी फेल हो जाओगे। सरकार ने तुम लोगों को सहूलियतें दी हैं, उनका फायदा उठाओ।’’
‘‘सरकार हम पर कोई अहसान नहीं कर रही है।’’
‘‘लेकिन...’’
‘‘मुझे तुम्हारा उपेदश नहीं चाहिए, प्लीज।’’
‘‘मिलिन्द सुनने की मनोदशा में नहीं था। मैं उसे काँटे की तरह चुभ रहा था। मैं उसके भले की ही बात कह रहा था लेकिन वह माने तब न ! मैं चाहता था कि मेरे कमरे में पढ़ाई की चर्चाएँ हों लेकिन यहाँ रात-दिन संगठन की बातें होती थीं। मुझे यह नहीं चाहिए था। हम पढ़ाई करने आए हैं, हमें बस पढ़ाई ही करनी चाहिए।
मिलिन्द ने सिगरेट सुलगाई। धुएँ की लहरें उठने लगीं। मुझे गुस्सा आ गया। जोर से चिल्लाने को जी हुआ ‘नो स्मोकिंग !’’ लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया। ज्यादा तानना भी ठीक नहीं। वह समझ गया कि मैं नाराज हो गया हूँ।
रोहिदास रूम से चला गया यह तो अच्छा ही हुआ। कभी-न-कभी यह होना ही था। आज ही हो गया।
मेरी नस-नस में द्वेष और विद्रोह की लहरें भड़कने लगी थीं-
‘मस्ती आ गई है। सरकार इन्हें सहूलियतें दे रही है और ये हैं कि बीड़ियाँ पी रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, मुफ्त के वजीफे लेते हैं। होस्टल में कचरा भरा हुआ है। थर्ड क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्हें आसानी से प्रवेश मिल जाता है और हम बुद्धिमान हैं, फिर भी प्रवेश नहीं। हम सवर्ण हैं, इसमें हमारा क्या दोष है ? जो गद्दी पर बैठते रहे हैं अब जूते के पास बैठे हैं और जो जूते के पास थे सिंहासन पर बैठे हैं। अच्छा होता यदि हम भी चमार होते ! सहूलियतें मिल जातीं। सरकार कमअक्ल लोगों को बढ़ावा दे रही है। सरकार ऐसे लोगों पर पैसा क्यों बरबाद करे ? दलित मतों के लिए सरकार इन्हें खुश कर रही है। मुझे लगता है कि इन सब अछूतों को इकट्ठा करके उन पर एक बम गिरा देना चाहिए।’
‘‘गुस्से में तुम कहीं सचमुच तो फाँसी नहीं लगा लोगे, इसी चिन्ता में मैं रात-भर नहीं सोया।’’ रोहिदास की बात में कड़वाहट नहीं थी
‘‘मैंने रात में कई बार उठकर देखा। यह तो आराम से खर्राटे भर रहा था।’’ मिलिन्द ने मजाक में कहा।
मुझसे भी रहा नहीं गया।
‘‘रात कहाँ सोए थे ?’’
‘‘गौतम गांगुर्डे के कमरे में। मैंने तो बस स्टैंड पर भी ऐसी कई रातें गुजारी हैं।’’ महार-चमारों में यह अच्छा है, कैसे भी जी लेते हैं !
मिलिन्द और रोहिदास सोने की तैयारी करने लगे। मैंने टोका-
‘‘लगता है, आज यहीं सोओगे ?’’
रोहिदास, ने सिर हिलाया-
‘‘कल से गांगुर्डे के कमरे में रहूंगा। आज उसके पास कुछ गेस्ट आए हैं, इसलिए वहाँ जगह नहीं है।’’
मैंने कुछ नहीं कहा। इस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए हम दोनों को चुप ही रहना चाहिए।
आँख कब लग गई, पता नहीं चला। कानाफूसी की आवाज से नींद उचटी। मिलिन्द और रोहिदास के बीच बातचीत हो रही थी। उनकी बातों से घटना का पता चल रहा था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book