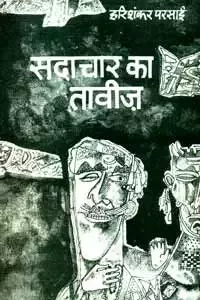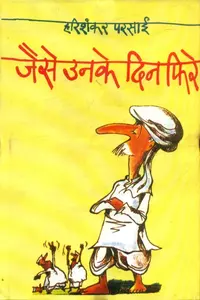|
हास्य-व्यंग्य >> तिरछी रेखाएँ तिरछी रेखाएँहरिशंकर परसाई
|
125 पाठक हैं |
||||||
हरिशंकर परसाई द्वारा हास्य-व्यंग्य पर आधारित पुस्तक...
Tirachhi Rekhayen
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
परसाई जी की रचनाएं राजनीति, साहित्य, भ्रष्टाचार, आजादी के बाद का ढोंग, आज के जीवन का अन्तर्विरोध, पाखंड और विसंगतियों को हमारे सामने इस तरह खोलती हैं जैसे कोई सर्जन चाकू से शरीर काट-काटकर गले अंग आपके सामने प्रस्तुत करता है। उसका व्यंग्य मात्र हँसाता नहीं है, वरन् तिलमिलाता है और सोचने को बरबस बाध्य कर देता है। कबीर जैसी उनकी अवधूत और निःसंग शैली उनकी एक विशिष्ट उपलब्धि है और उसी के द्वारा उनका जीवन चिंतर मुखर हुआ है। उनके जैसा मानवीय संवेदना में डूबा हुआ कलाकार रोज पैदा नहीं होता।
आजादी के पहले का हिंदुस्तान जानने के लिए सिर्फ प्रेमचन्द्र पढ़ना ही काफी है, उसी तरह आजादी के बाद की पूरी दस्तावेज परसाई की रचनाओं में सुरक्षित है। चश्मा लगाकर ‘रामचंद्रिका’ पढ़ाने वाले पेशेवर हिंदी के ठेकेदारों के बावजूद, परसाई का स्थान हिन्दी में हमेशा-हमेशा के लिए सुरक्षित है।
आजादी के पहले का हिंदुस्तान जानने के लिए सिर्फ प्रेमचन्द्र पढ़ना ही काफी है, उसी तरह आजादी के बाद की पूरी दस्तावेज परसाई की रचनाओं में सुरक्षित है। चश्मा लगाकर ‘रामचंद्रिका’ पढ़ाने वाले पेशेवर हिंदी के ठेकेदारों के बावजूद, परसाई का स्थान हिन्दी में हमेशा-हमेशा के लिए सुरक्षित है।
व्यंग्य क्यों? कैसे? किस लिए?
मैं व्यंग्य लेखक माना जाता हूँ। व्यंग्य को लेकर जितना भ्रम हिन्दी में है, उतना किसी और विधा को लेकर नहीं। समीक्षकों ने भी इसकी लगातार उपेक्षा की है। अभी तक व्यंग्य की समीक्षा की भाषा ही नहीं बनी। ‘मजा आ गया’ से लेकर ‘बखिया उधेड़ दी’ तक कुछ फ़िकरे इस पर चिपका कर समीक्षा की इतिश्री समझ ली जाती है। अकसर विनोद, हास्य मखौल से व्यंग्य को अलग करके नहीं देखा जाता। मेरी ही कोई रचना पढ़कर प्रबुद्ध पाठक भी कह देता है-बड़ा मजा आया, जब कि मैंने खिजाने के लिए वह चीज़ लिखी है।
आदमी कब हँसता है ? इस सम्बन्ध में बड़ी दिलचस्प और विभिन्न धारणाएँ हैं। एक विचार यह है कि जब आदमी हँसता है, तब उसके मन में मैल नहीं होता। हँसने के क्षणभर पहले उसके मन में मैल हो सकता है और हँसी के क्षणभर बाद भी। पर जिस क्षण वह हँसता है, उसके मन में किसी के प्रति मैल नहीं होता। फिर जिसका हाज़मा अच्छा हो वही हँस सकता है। कब्ज का मरीज़ मुश्किल से हँसता है। फिर जब मनुष्य को चैन की (well being) अनुभूति होती है, तब वह हँसता है। बिना चैन की हँसी खिन्न हँसी होती है, जैसी पंडित नेहरू की अन्तिम वर्षों में हो गयी थी।
आदमी हँसता क्यों है ? परम्परा से हर समाज की कुछ संगतियाँ होती हैं, सामंजस्य होते हैं, अनुपात होते हैं। ये व्यक्ति और समाज दोनों के होते हैं। जब यह संगति गड़बड़ होती है तब चेतना में चमक पैदा होती है। इस चमक से हँसी भी आ सकती है और चेतना में हलचल भी पैदा हो सकती है। शरीर में कितनी बड़ी नाक हो इसका एक अनुपात मानस में बना हुआ है। पर अगर किसी की बहुत मोटी नाक हो तो लोग कहते हैं-अरे, यह तो नाक की जगह आलूबड़ा रखे हैं-और हँस पड़ते हैं। साइकिल पर एक आदमी बैठे, यह संगति है। दो को बरदास्त कर लिया जाता है, पर एक साइकिल पर तीन सवार हों और वे गिर पड़ें तो उनकी चोट के प्रति सहानुभूति नहीं होगी बल्कि दर्शक हँस पड़ेंगे-अच्छे गिरे साले। हमारे यहाँ कंजी आँख बुरी मानी जाती है। कंजी आँख वाले पर लोग हँसते हैं। कहावत है-
आदमी कब हँसता है ? इस सम्बन्ध में बड़ी दिलचस्प और विभिन्न धारणाएँ हैं। एक विचार यह है कि जब आदमी हँसता है, तब उसके मन में मैल नहीं होता। हँसने के क्षणभर पहले उसके मन में मैल हो सकता है और हँसी के क्षणभर बाद भी। पर जिस क्षण वह हँसता है, उसके मन में किसी के प्रति मैल नहीं होता। फिर जिसका हाज़मा अच्छा हो वही हँस सकता है। कब्ज का मरीज़ मुश्किल से हँसता है। फिर जब मनुष्य को चैन की (well being) अनुभूति होती है, तब वह हँसता है। बिना चैन की हँसी खिन्न हँसी होती है, जैसी पंडित नेहरू की अन्तिम वर्षों में हो गयी थी।
आदमी हँसता क्यों है ? परम्परा से हर समाज की कुछ संगतियाँ होती हैं, सामंजस्य होते हैं, अनुपात होते हैं। ये व्यक्ति और समाज दोनों के होते हैं। जब यह संगति गड़बड़ होती है तब चेतना में चमक पैदा होती है। इस चमक से हँसी भी आ सकती है और चेतना में हलचल भी पैदा हो सकती है। शरीर में कितनी बड़ी नाक हो इसका एक अनुपात मानस में बना हुआ है। पर अगर किसी की बहुत मोटी नाक हो तो लोग कहते हैं-अरे, यह तो नाक की जगह आलूबड़ा रखे हैं-और हँस पड़ते हैं। साइकिल पर एक आदमी बैठे, यह संगति है। दो को बरदास्त कर लिया जाता है, पर एक साइकिल पर तीन सवार हों और वे गिर पड़ें तो उनकी चोट के प्रति सहानुभूति नहीं होगी बल्कि दर्शक हँस पड़ेंगे-अच्छे गिरे साले। हमारे यहाँ कंजी आँख बुरी मानी जाती है। कंजी आँख वाले पर लोग हँसते हैं। कहावत है-
सौ में सूर सहस्त्र में काना,
सवा लाख में ऐंचक ताना।
ऐंचक ताना करे पुकार,
मैं कंजे से खाई हार।
सवा लाख में ऐंचक ताना।
ऐंचक ताना करे पुकार,
मैं कंजे से खाई हार।
पर कंजी आँखें पश्चिम में अच्छी मानी जाती हैं। आमतौर पर पतले ओंठ सुन्दर माने जाते हैं पर नीग्रो लोगों में अच्छे मोटे ओंठ भी अच्छे लगते हैं। भारत में किसी के नीग्रो जैसे मोटे ओंठ हों तो लोग हँसेंगे क्योंकि सौंदर्य बोध की संगति बिगड़ती है।
लोग किसी भी बात पर हँसते हैं। हलकी, मामूली विसंगति पर भी हँस देते हैं। आदमी अगर घोड़े सरीखा हिनहिनाए तो इस पर भी हँस देते हैं। दीवाली पर कुत्ते की दुम में पटाखे की लड़ी बाँधकर उसमें कुछ लोग आग लगा देते हैं। बेचारा कुत्ता तो मृत्यु भय से भागता और चीखता है, पर लोग हँसते हैं।
पर व्यंग्य में जरूरी नहीं कि हँसी आये ही। मार्क ट्वेन ने लिखा है-यदि कोई भूखे कुत्ते को रोटी खिलाए तो वह उसे काटेगा नहीं। मनुष्य और कुत्ते में यही खास फ़र्क है। इस कथन से हँसी नहीं आती पर व्यंग्य की वह करारी यह चोट चेतना पर करता है कि पाठक पहले तो भौंचक रह जाता है और फिर सोचने लगता है।
व्यंग्य के साथ हँसी भी आती है, पर वह दूसरे प्रकार की होती है। मेरी ही एक लघु कथा है-संसद में एक सदस्य ने कहा कि अमुक जगह पुलिस की गोली से ग्यारह आदमी मारे गये। गृहमन्त्री इसका जवाब दें। गृहमन्त्री बड़ी शान्ति से उठे। जिन्हें रोज गोली चलवानी है वे कब तक अशान्त रहेंगे। गृहमन्त्री ने जवाब दिया-गोली का कारखाना जनता के पैसे से चलता है। जनता कै पैसे से जो सामान बनता है, उसे जनता के ही काम आना चाहिए। अब जनतान्त्रिक असूल में यह बात पूरी तरह संगत है। पर यह कितनी बड़ी विडम्बना पैदा करती है और संसदीय प्रणाली पर चोट करती है। इस लघुकथा से हँसी जरूर आती है पर यह हँसी और किस्म की होती है और सोचने को बाध्य करती है।
व्यंग्य लेखन एक गम्भीर कर्म है। कम से कम मेरे लिए। सवाल यह है कि कोई लेखक अपने युग की विसंगतियों को कितने गहरे से खोजता है। उस विसंगति की व्यापकता क्या है और वह जीवन में कितनी अहमियत रखती है मात्र व्यक्ति की ऊपरी विसंगति-शरीर रचना की, व्यवहार की, बात के लहजे की एक चीज़ है। और व्यक्ति तथा समाज के जीवन की भीतरी तहों में जाकर विसंगति खोजना, उन्हें अर्थ देना तथा उसे सशक्त विरोधाभास से पृथक करके जीवन से साक्षात्कार कराना दूसरी बात है। सच्चा व्यंग्य जीवन की समीक्षा होता है। वह मनुष्य को सोचने के लिए बाध्य करता है। अपने से साक्षात्कार करता है। चेतना में हलचल पैदा करता है और जीवन में व्याप्त मिथ्याचार, पाखंड असामंजस्य और अन्याय से लड़ने के लिए उसे तैयार करता है।
जोनाथन स्विफ्ट कहता है-मैं मनुष्य को अपमानित करने और उसे नीचा दिखाने के लिए लिखता हूँ। परन्तु मार्क ट्वेन कहता है-मैं बुनियादी तौर पर एक शिक्षक हूँ। मेरा खयाल है, कोई भी सच्चा व्यंग्य लेखक मनुष्य को नीचा नहीं दिखाना चाहता। व्यंग्य मानव सहानुभूति से पैदा होता है। वह मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाना चाहता है। वह उससे कहता है-तू अधिक सच्चा, न्यायी मानवीय बन। यदि मनुष्य के प्रति व्यंग्यकार को आशा नहीं है, यदि वह जीवन के प्रति कनसर्न्ड नहीं है तो वह क्यों रोता है उसकी कमजोरियों पर। जो यह कहते हैं कि व्यंग्य लेखक निर्मम, कठोर और मनुष्य विरोधी होता है, उसे बुराई ही बुराई दिखती है, तो मैं जवाब देता हूँ कि डॉक्टर के पास जो लोग जाते हैं उन्हें वह रोग बताता है। तो क्या डॉक्टर कठोर है ? अमानवीय है ? अगर डॉक्टर रोग का निदान न कर और अच्छा ही अच्छा कहे तो रोगी मर जायेगा। जीवन की कमजोरियों का निदान करना कठोर होना नहीं है।
अच्छे व्यंग्य में करुणा की अंतर्धारा होती है। चेखव में शायद यह बात सबसे साफ़ है। चेखव की एक कहानी है-बाबू की मौत। इस कहानी को पढ़ते-पढ़ते हँसी आती है पर अन्त में मन करुणा से भर उठता है। जिस बात पर कहानी का ताना-बाना चेखव ने बुना वह यह है-
थियेटर में एक बाबू नाटक देख रहा है। उसके ठीक सामने उसका बॉस बैठा है। बॉस के चाँद है। बाबू को छींक आती है और उसे लगता है कि उसकी छींक के छींटे साहब की चाँद पर पड़ गये हैं। वह घबराता है और इंटरवल में साहब से माफी माँगता है-साहब माफ़ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गयी। मैंने जान बूझ कर गुस्ताखी नहीं की। अब मजा यह है कि साहब की चाँद पर छींटे पड़े ही नहीं हैं। वह नहीं जानता कि बाबू माफी किस बात की मांग रहा है। वह उसे डाँटता है-क्या बक-बक लगा रखी है। भागो यहाँ से। इधर बाबू समझता है कि साहब ज्यादा नाराज है। वह खेल छूटने पर फिर माफी माँगता है-साहब मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे जुखाम हो गया है। मैंने जानबूझ कर वैसा नहीं किया है। साहब फिर उसे डाँट कर भगा देता है। तीन दिन तक यह क्रम चलता है। बाबू माफी माँगता है, पर साहब नहीं जानते कि माफी किस बात की माँग रहा है। वह अधिकाधिक खीज कर उसे भगाता है। इधर बाबू समझता है कि साहब को बड़े छींटे पड़े होंगे तभी नाराज है। यहाँ तक तो कहानी में एक कॉमिक का वातावरण रहता है। पर जब साहब उसे चपरासी से बाहर निकलवा देता है तब वह सोचता है-अब नौकरी गयी। मेरी बीवी है। तीन बच्चे हैं। इनका पालन कैसे होगा ?
इसी घबराहट में वह घर आता है। कुर्सी पर बैठता है और उसके प्राण निकल जाते हैं।
कैसा करुण प्रसंग है। कहानी में चेखव ने इस कठोर नौकरशाही पर चोट की है जिसमें साहब अहंकार के कारण बाबू से पूछता तक नहीं कि तू माफी क्यों माँग रहा है। सिर्फ इतना पूछ लेता तो बाबू की जान नहीं जाती।
व्यंग्य के सम्बन्ध में कुछ बातें मैंने यहाँ कहीं, इस मकसद से कि व्यंग्य का मर्म समझने में इनसे कुछ सहायता मिलेगी।
लोग किसी भी बात पर हँसते हैं। हलकी, मामूली विसंगति पर भी हँस देते हैं। आदमी अगर घोड़े सरीखा हिनहिनाए तो इस पर भी हँस देते हैं। दीवाली पर कुत्ते की दुम में पटाखे की लड़ी बाँधकर उसमें कुछ लोग आग लगा देते हैं। बेचारा कुत्ता तो मृत्यु भय से भागता और चीखता है, पर लोग हँसते हैं।
पर व्यंग्य में जरूरी नहीं कि हँसी आये ही। मार्क ट्वेन ने लिखा है-यदि कोई भूखे कुत्ते को रोटी खिलाए तो वह उसे काटेगा नहीं। मनुष्य और कुत्ते में यही खास फ़र्क है। इस कथन से हँसी नहीं आती पर व्यंग्य की वह करारी यह चोट चेतना पर करता है कि पाठक पहले तो भौंचक रह जाता है और फिर सोचने लगता है।
व्यंग्य के साथ हँसी भी आती है, पर वह दूसरे प्रकार की होती है। मेरी ही एक लघु कथा है-संसद में एक सदस्य ने कहा कि अमुक जगह पुलिस की गोली से ग्यारह आदमी मारे गये। गृहमन्त्री इसका जवाब दें। गृहमन्त्री बड़ी शान्ति से उठे। जिन्हें रोज गोली चलवानी है वे कब तक अशान्त रहेंगे। गृहमन्त्री ने जवाब दिया-गोली का कारखाना जनता के पैसे से चलता है। जनता कै पैसे से जो सामान बनता है, उसे जनता के ही काम आना चाहिए। अब जनतान्त्रिक असूल में यह बात पूरी तरह संगत है। पर यह कितनी बड़ी विडम्बना पैदा करती है और संसदीय प्रणाली पर चोट करती है। इस लघुकथा से हँसी जरूर आती है पर यह हँसी और किस्म की होती है और सोचने को बाध्य करती है।
व्यंग्य लेखन एक गम्भीर कर्म है। कम से कम मेरे लिए। सवाल यह है कि कोई लेखक अपने युग की विसंगतियों को कितने गहरे से खोजता है। उस विसंगति की व्यापकता क्या है और वह जीवन में कितनी अहमियत रखती है मात्र व्यक्ति की ऊपरी विसंगति-शरीर रचना की, व्यवहार की, बात के लहजे की एक चीज़ है। और व्यक्ति तथा समाज के जीवन की भीतरी तहों में जाकर विसंगति खोजना, उन्हें अर्थ देना तथा उसे सशक्त विरोधाभास से पृथक करके जीवन से साक्षात्कार कराना दूसरी बात है। सच्चा व्यंग्य जीवन की समीक्षा होता है। वह मनुष्य को सोचने के लिए बाध्य करता है। अपने से साक्षात्कार करता है। चेतना में हलचल पैदा करता है और जीवन में व्याप्त मिथ्याचार, पाखंड असामंजस्य और अन्याय से लड़ने के लिए उसे तैयार करता है।
जोनाथन स्विफ्ट कहता है-मैं मनुष्य को अपमानित करने और उसे नीचा दिखाने के लिए लिखता हूँ। परन्तु मार्क ट्वेन कहता है-मैं बुनियादी तौर पर एक शिक्षक हूँ। मेरा खयाल है, कोई भी सच्चा व्यंग्य लेखक मनुष्य को नीचा नहीं दिखाना चाहता। व्यंग्य मानव सहानुभूति से पैदा होता है। वह मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाना चाहता है। वह उससे कहता है-तू अधिक सच्चा, न्यायी मानवीय बन। यदि मनुष्य के प्रति व्यंग्यकार को आशा नहीं है, यदि वह जीवन के प्रति कनसर्न्ड नहीं है तो वह क्यों रोता है उसकी कमजोरियों पर। जो यह कहते हैं कि व्यंग्य लेखक निर्मम, कठोर और मनुष्य विरोधी होता है, उसे बुराई ही बुराई दिखती है, तो मैं जवाब देता हूँ कि डॉक्टर के पास जो लोग जाते हैं उन्हें वह रोग बताता है। तो क्या डॉक्टर कठोर है ? अमानवीय है ? अगर डॉक्टर रोग का निदान न कर और अच्छा ही अच्छा कहे तो रोगी मर जायेगा। जीवन की कमजोरियों का निदान करना कठोर होना नहीं है।
अच्छे व्यंग्य में करुणा की अंतर्धारा होती है। चेखव में शायद यह बात सबसे साफ़ है। चेखव की एक कहानी है-बाबू की मौत। इस कहानी को पढ़ते-पढ़ते हँसी आती है पर अन्त में मन करुणा से भर उठता है। जिस बात पर कहानी का ताना-बाना चेखव ने बुना वह यह है-
थियेटर में एक बाबू नाटक देख रहा है। उसके ठीक सामने उसका बॉस बैठा है। बॉस के चाँद है। बाबू को छींक आती है और उसे लगता है कि उसकी छींक के छींटे साहब की चाँद पर पड़ गये हैं। वह घबराता है और इंटरवल में साहब से माफी माँगता है-साहब माफ़ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गयी। मैंने जान बूझ कर गुस्ताखी नहीं की। अब मजा यह है कि साहब की चाँद पर छींटे पड़े ही नहीं हैं। वह नहीं जानता कि बाबू माफी किस बात की मांग रहा है। वह उसे डाँटता है-क्या बक-बक लगा रखी है। भागो यहाँ से। इधर बाबू समझता है कि साहब ज्यादा नाराज है। वह खेल छूटने पर फिर माफी माँगता है-साहब मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे जुखाम हो गया है। मैंने जानबूझ कर वैसा नहीं किया है। साहब फिर उसे डाँट कर भगा देता है। तीन दिन तक यह क्रम चलता है। बाबू माफी माँगता है, पर साहब नहीं जानते कि माफी किस बात की माँग रहा है। वह अधिकाधिक खीज कर उसे भगाता है। इधर बाबू समझता है कि साहब को बड़े छींटे पड़े होंगे तभी नाराज है। यहाँ तक तो कहानी में एक कॉमिक का वातावरण रहता है। पर जब साहब उसे चपरासी से बाहर निकलवा देता है तब वह सोचता है-अब नौकरी गयी। मेरी बीवी है। तीन बच्चे हैं। इनका पालन कैसे होगा ?
इसी घबराहट में वह घर आता है। कुर्सी पर बैठता है और उसके प्राण निकल जाते हैं।
कैसा करुण प्रसंग है। कहानी में चेखव ने इस कठोर नौकरशाही पर चोट की है जिसमें साहब अहंकार के कारण बाबू से पूछता तक नहीं कि तू माफी क्यों माँग रहा है। सिर्फ इतना पूछ लेता तो बाबू की जान नहीं जाती।
व्यंग्य के सम्बन्ध में कुछ बातें मैंने यहाँ कहीं, इस मकसद से कि व्यंग्य का मर्म समझने में इनसे कुछ सहायता मिलेगी।
-हरिशंकर परसाई
आत्मकथ्य
गर्दिश के दिन
लिखने बैठ गया हूँ पर नहीं जानता संपादक की मंशा क्या है और पाठक क्या चाहते हैं, क्यों आखिर वे उन दिनों में झाँकना चाहते हैं, जो लेखक के अपने हैं और जिनपर शायद वह परदा डाल चुका है। अपने गर्दिश के दिनों को, जो मेरे नामधारी एक आदमी के थे, मैं किस हैसियत से फिर जीऊँ ?-उस आदमी की हैसियत से या लेखक की हैसियत से ? लेखक की हैसियत से गर्दिश को फिर जी लेने और अभिव्यक्त कर देने में मनुष्य और लेखक, दोनों की मुक्ति है। इसमें मैं कोई ‘भोक्ता’ और ‘सर्जक’ की निःसंगता की बात नहीं दुहरा रहा हूँ। पर गर्दिश को फिर याद करने, उसे जीने में दारुण कष्ट है। समय के सींगों को मैंने मोड़ दिया था। अब फिर उन सींगों को सीधा करके कहूँ-आ बैल, मुझे मार !
गर्दिश कभी थी अब नहीं है, आगे नहीं होगी-यह गलत है। गर्दिश का सिलसिला बदस्तूर है, मैं निहायत बेचैन मन का संवेदनशील आदमी हूँ। मुझे चैन कभी मिल ही नहीं सकता। इसलिए गर्दिश नियति है।
हाँ, यादें बहुत हैं। पाठक को शायद इसमें दिलचस्पी हो कि यह जो हरिशंकर परसाई नाम का आदमी है, जो हँसता है, जिसमें मस्ती है, जो ऐसा तीखा है कटु है-इसकी अपनी जिन्दगी कैसी रही है ? यह कब गिरा फिर कब उठा ? कैसे टूटा ? कैसे फिर से जुड़ा ? यह एक निहायत कटु, निर्मम और धोबीपछाड़ आदमी है।
संयोग कि बचपन की सबसे तीखी याद ‘प्लेग’ की है। 1936 या 37 होगा। मैं शायद आठवीं का छात्र था। कस्बे में प्लेग पड़ी थी। आबादी घर छोड़ जंगल में टपरे बना कर रहने चली गयी थी। हम नहीं गये थे। माँ सख्त बीमार थी। उन्हें लेकर जंगल नहीं जाया जा सकता था। भाँय-भाँय करते पूरे आस-पास में हमारे घर ही चहल-पहल थी। काली रातें। इनमें हमारे घर जलने वाले कंदील। मुझे इन कंदीलों से डर लगता था। कुत्ते तक बस्ती छोड़ गये थे, रात के सन्नाटे में हमारी आवाजें हमें ही डरावनी लगती थीं। रात को मरणासन्न माँ के सामने हम लोग आरती गाते-जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे। गाते गाते पिताजी सिसकने लगते, माँ बिलख कर हम बच्चों को हृदय से चिपटा लेती और हम भी रोने लगते। रोज का यह नियम था। फिर रात को पिताजी, चाचा और दो एक रिश्तेदार लाठी-बल्लम लेकर घर के चारों तरफ घूम-घूम कर पहरा देते। ऐसे भयकारी, त्रासदायक वातावरण में एक रात तीसरे पहर माँ की मृत्यु हो गयी। कोलाहल और विलाप शुरू हो गया। कुछ कुत्ते भी सिमट कर आ गये और योग देने लगे।
पाँच भाई-बहनों में माँ की मृत्यु का अर्थ मैं ही समझाता था-सबसे बड़ा था।
प्लेग की वे रातें मेरे मन में गहरे उतरी हैं। जिस, आंतक, अनिश्चय निराशा और भय के बीच हम जी रहे थे, उसके सही अकंन के लिए बहुत पन्ने चाहिए। यह भी कि पिता के सिवा हम कोई टूटे नहीं थे। वह टूट गये थे। वह इसके बाद भी 5-6 साल जिये, लेकिन लगातार बीमार, हताश, निष्क्रिय और अपने से ही डरते हुए। धंधा ठप्प। जमा-पूँजी खाने लगे। मेरे मैट्रिक पास होने की राह देखी जाने लगी। समझने लगा था कि पिताजी भी अब जाते ही हैं बीमारी की हालत में उन्होंने एक बहन की शादी कर ही दी थी-बहुत मनहूस उत्सव था वह। मैं बराबर समझ रहा था कि मेरा बोझ कम किया जा रहा है। फिर अभी दो छोटी बहनें और एक भाई थे।
मैं तैयार होने लगा। खूब पढ़ने वाला, खूब खेलने वाला और खूब खाने वाला मैं शुरू से था। पढ़ने और खेलने में मैं सब भूल जाता। मैट्रिक हुआ, जंगल विभाग में नौकरी मिली। जंगल में सरकारी टपरे में रहता। ईंटें रखकर, उन पर पटिये जमा कर बिस्तार लगाता, नीचे जमीन चूहों ने पोली कर दी थी। रात भर नीचे चूहे धमाचौकड़ी करते रहते और मैं सोता रहता। कभी चूहे ऊपर आ जाते तो नींद टूट जाती पर मैं फिर सो जाता। छह महीने धमाचौकड़ी करते चूहों पर मैं सोया।
बेचारा परसाई ?
नहीं, नहीं, मैं खूब मस्त था। दिन भर काम। शाम को जंगल में घुमाई फिर हाथ से बना कर खाया गया भरपेट भोजन-शुद्ध घी और दूध। और चूहों ने बड़ा उपकार किया। ऐसी आदत डाली कि आगे की जिन्दगी में भी तरह-तरह के चूहे मेरे नीचे ऊधम करते रहे हैं, साँप तक सर्राते रहे हैं, मगर मैं पटिया बिछा कर पटिये पर सोता रहा हूँ। चूहों ने ही नहीं, मनुष्यनुमा बिच्छुओं और साँपों ने भी मुझे बहुत काटा है-पर ‘जहर मोहरा’ मुझे शुरू में ही मिल गया। इसलिए ‘बेचारा परसाई’ का मौका ही नहीं आने दिया। उसी उम्र से दिखाऊ सहानुभूति से मुझे बेहद नफरत है। अभी भी दिखाऊ सहानुभूति वाले को चाँटा मार देने की इच्छा होती है जब्त कर जाता हूँ वरना कई शुभचिंतक पिट जाते।
फिर स्कूल मास्टरी। फिर टीचर्स ट्रेनिंग और नौकरी की तलाश-उधर पिताजी मृत्यु के नजदीक। भाई पढ़ाई रोककर उनकी सेवा में। बहनें बड़ी बहन के साथ हम शिक्षण की शिक्षा ले रहे हैं।
फिर नौकरी की तलाश। एक विद्या मुझे और आ गयी थी-बिना टिकट सफर करना। जबलपुर से इटारसी, टिमरनी, खंडवा, इन्दौर, देवास बार-बार चक्कर लगाने पड़ते। पैसे थे नहीं। मैं बिना टिकट बेखटके गाड़ी में बैठ जाता। तरकीबें बचने की बहुत आ गयी थीं। पकड़ा जाता तो अच्छा अंग्रेजी में अपनी मुसीबत का बखान करता। अंग्रेजी के माध्यम से मुसीबात बाबुओं को प्रभावित कर देती और वे कहते-लेट्स हेल्प दि पूअर बॉय।
दूसरी विद्या सीखी-उधार माँगने की। मैं बिल्कुल निःसंकोच भाव से किसी से भी उधार माँग लेता। अभी भी इस विद्या में सिद्ध हूँ।
तीसरी चीज सीखी बेफिक्री ! जो होना होगा, होगा, क्या होगा ? ठीक ही होगा। मेरी एक बुआ थी। गरीब, जिन्दगी गर्दिश भरी, मगर अपार जीवन-शक्ति थी उसमें। खाना बनने लगता तो उनकी बहू कहती-बाई, न दाल ही है न तरकारी। बुआ कहती-चल, चिन्ता नहीं। राह मोहल्ले में निकलती और जहाँ उसे छप्पर पर सब्जी दिख जाती, वहीं अपनी हम उम्र मालकिन से कहती-ए कौशल्या तेरी तोरई अच्छी आ गयी है। जरा दो मुझे तोड़ के दे। और खुद तोड़ लेती। बहू से कहती-ले बना डाल, जरा पानी जादा डाल देना। मैं यहाँ-वहाँ से मारा हुआ उसके पास जाता तो वह कहती-चल, कोई चिन्ता नहीं, कुछ खा ले।
उसका यह वाक्य मेरे लिए ताकत बना-कोई चिन्ता नहीं।
गर्दिश कभी थी अब नहीं है, आगे नहीं होगी-यह गलत है। गर्दिश का सिलसिला बदस्तूर है, मैं निहायत बेचैन मन का संवेदनशील आदमी हूँ। मुझे चैन कभी मिल ही नहीं सकता। इसलिए गर्दिश नियति है।
हाँ, यादें बहुत हैं। पाठक को शायद इसमें दिलचस्पी हो कि यह जो हरिशंकर परसाई नाम का आदमी है, जो हँसता है, जिसमें मस्ती है, जो ऐसा तीखा है कटु है-इसकी अपनी जिन्दगी कैसी रही है ? यह कब गिरा फिर कब उठा ? कैसे टूटा ? कैसे फिर से जुड़ा ? यह एक निहायत कटु, निर्मम और धोबीपछाड़ आदमी है।
संयोग कि बचपन की सबसे तीखी याद ‘प्लेग’ की है। 1936 या 37 होगा। मैं शायद आठवीं का छात्र था। कस्बे में प्लेग पड़ी थी। आबादी घर छोड़ जंगल में टपरे बना कर रहने चली गयी थी। हम नहीं गये थे। माँ सख्त बीमार थी। उन्हें लेकर जंगल नहीं जाया जा सकता था। भाँय-भाँय करते पूरे आस-पास में हमारे घर ही चहल-पहल थी। काली रातें। इनमें हमारे घर जलने वाले कंदील। मुझे इन कंदीलों से डर लगता था। कुत्ते तक बस्ती छोड़ गये थे, रात के सन्नाटे में हमारी आवाजें हमें ही डरावनी लगती थीं। रात को मरणासन्न माँ के सामने हम लोग आरती गाते-जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे। गाते गाते पिताजी सिसकने लगते, माँ बिलख कर हम बच्चों को हृदय से चिपटा लेती और हम भी रोने लगते। रोज का यह नियम था। फिर रात को पिताजी, चाचा और दो एक रिश्तेदार लाठी-बल्लम लेकर घर के चारों तरफ घूम-घूम कर पहरा देते। ऐसे भयकारी, त्रासदायक वातावरण में एक रात तीसरे पहर माँ की मृत्यु हो गयी। कोलाहल और विलाप शुरू हो गया। कुछ कुत्ते भी सिमट कर आ गये और योग देने लगे।
पाँच भाई-बहनों में माँ की मृत्यु का अर्थ मैं ही समझाता था-सबसे बड़ा था।
प्लेग की वे रातें मेरे मन में गहरे उतरी हैं। जिस, आंतक, अनिश्चय निराशा और भय के बीच हम जी रहे थे, उसके सही अकंन के लिए बहुत पन्ने चाहिए। यह भी कि पिता के सिवा हम कोई टूटे नहीं थे। वह टूट गये थे। वह इसके बाद भी 5-6 साल जिये, लेकिन लगातार बीमार, हताश, निष्क्रिय और अपने से ही डरते हुए। धंधा ठप्प। जमा-पूँजी खाने लगे। मेरे मैट्रिक पास होने की राह देखी जाने लगी। समझने लगा था कि पिताजी भी अब जाते ही हैं बीमारी की हालत में उन्होंने एक बहन की शादी कर ही दी थी-बहुत मनहूस उत्सव था वह। मैं बराबर समझ रहा था कि मेरा बोझ कम किया जा रहा है। फिर अभी दो छोटी बहनें और एक भाई थे।
मैं तैयार होने लगा। खूब पढ़ने वाला, खूब खेलने वाला और खूब खाने वाला मैं शुरू से था। पढ़ने और खेलने में मैं सब भूल जाता। मैट्रिक हुआ, जंगल विभाग में नौकरी मिली। जंगल में सरकारी टपरे में रहता। ईंटें रखकर, उन पर पटिये जमा कर बिस्तार लगाता, नीचे जमीन चूहों ने पोली कर दी थी। रात भर नीचे चूहे धमाचौकड़ी करते रहते और मैं सोता रहता। कभी चूहे ऊपर आ जाते तो नींद टूट जाती पर मैं फिर सो जाता। छह महीने धमाचौकड़ी करते चूहों पर मैं सोया।
बेचारा परसाई ?
नहीं, नहीं, मैं खूब मस्त था। दिन भर काम। शाम को जंगल में घुमाई फिर हाथ से बना कर खाया गया भरपेट भोजन-शुद्ध घी और दूध। और चूहों ने बड़ा उपकार किया। ऐसी आदत डाली कि आगे की जिन्दगी में भी तरह-तरह के चूहे मेरे नीचे ऊधम करते रहे हैं, साँप तक सर्राते रहे हैं, मगर मैं पटिया बिछा कर पटिये पर सोता रहा हूँ। चूहों ने ही नहीं, मनुष्यनुमा बिच्छुओं और साँपों ने भी मुझे बहुत काटा है-पर ‘जहर मोहरा’ मुझे शुरू में ही मिल गया। इसलिए ‘बेचारा परसाई’ का मौका ही नहीं आने दिया। उसी उम्र से दिखाऊ सहानुभूति से मुझे बेहद नफरत है। अभी भी दिखाऊ सहानुभूति वाले को चाँटा मार देने की इच्छा होती है जब्त कर जाता हूँ वरना कई शुभचिंतक पिट जाते।
फिर स्कूल मास्टरी। फिर टीचर्स ट्रेनिंग और नौकरी की तलाश-उधर पिताजी मृत्यु के नजदीक। भाई पढ़ाई रोककर उनकी सेवा में। बहनें बड़ी बहन के साथ हम शिक्षण की शिक्षा ले रहे हैं।
फिर नौकरी की तलाश। एक विद्या मुझे और आ गयी थी-बिना टिकट सफर करना। जबलपुर से इटारसी, टिमरनी, खंडवा, इन्दौर, देवास बार-बार चक्कर लगाने पड़ते। पैसे थे नहीं। मैं बिना टिकट बेखटके गाड़ी में बैठ जाता। तरकीबें बचने की बहुत आ गयी थीं। पकड़ा जाता तो अच्छा अंग्रेजी में अपनी मुसीबत का बखान करता। अंग्रेजी के माध्यम से मुसीबात बाबुओं को प्रभावित कर देती और वे कहते-लेट्स हेल्प दि पूअर बॉय।
दूसरी विद्या सीखी-उधार माँगने की। मैं बिल्कुल निःसंकोच भाव से किसी से भी उधार माँग लेता। अभी भी इस विद्या में सिद्ध हूँ।
तीसरी चीज सीखी बेफिक्री ! जो होना होगा, होगा, क्या होगा ? ठीक ही होगा। मेरी एक बुआ थी। गरीब, जिन्दगी गर्दिश भरी, मगर अपार जीवन-शक्ति थी उसमें। खाना बनने लगता तो उनकी बहू कहती-बाई, न दाल ही है न तरकारी। बुआ कहती-चल, चिन्ता नहीं। राह मोहल्ले में निकलती और जहाँ उसे छप्पर पर सब्जी दिख जाती, वहीं अपनी हम उम्र मालकिन से कहती-ए कौशल्या तेरी तोरई अच्छी आ गयी है। जरा दो मुझे तोड़ के दे। और खुद तोड़ लेती। बहू से कहती-ले बना डाल, जरा पानी जादा डाल देना। मैं यहाँ-वहाँ से मारा हुआ उसके पास जाता तो वह कहती-चल, कोई चिन्ता नहीं, कुछ खा ले।
उसका यह वाक्य मेरे लिए ताकत बना-कोई चिन्ता नहीं।
गर्दिश फिर गर्दिश !
होशंगाबाद शिक्षा अधिकारी से नौकरी माँगने गये। निराश हुए। स्टेशन पर इटारसी के लिए गाड़ी पकड़ने के लिए बैठा था पास में एक रुपया था जो कहीं गिर गया था। इटारसी तो बिना टिकट चला जाता। पर खाऊँ क्या ? दूसरे महायुद्ध का जमाना। गाड़ियाँ बहुत लेट होती थीं। पेट खाली। पानी से बार-बार भरता। आखिर बेंच पर लेट गया। 14 घंटे हो गये। एक किसान परिवार पास आकर बैठ गया। टोकरे में अपने खेत के खरबूजे थे, मैं उस वक्त चोरी भी कर सकता था। किसान खरबूजा काटने लगे। मैंने कहा-तुम्हारे ही खेत के होंगे। बड़े अच्छे हैं। किसान ने कहा-सब नर्मदा मैया की किरपा है भैया ! शक्कर की तरह हैं। लो खाके देखो। उसने दो बड़ी फाँकें दीं। मैंने कम-से-कम छिलका छोड़ कर खा लिया। पानी पिया। तभी गाड़ी आयी और हम खिड़की से घुस गये।
नौकरी मिली जबलपुर के सरकारी स्कूल में। किराये तक के पैसे नहीं। अध्यापक महोदय ने दरी में कपड़े बाँधे और बिना टिकट चढ़ गये गाड़ी में। सामान के कारण इस बार थोड़ा खटका था। पास में कलेक्टर का खानसामा बैठा था। बातचीत चलने लगी। आदमी मुझे अच्छा लगा। जबलपुर आने लगा तो मैंने उसे अपनी समस्या बतायी। उसने कहा-चिन्ता मत करो। सामान मुझे दो। मैं बाहर राह देखूँगा। तुम कहीं पानी पीने के बहाने सींखचों के पास पहुँच जाना। नल सींखचों के पास ही हैं। वहाँ सींखचों को उखाड़ कर निकलने की जगह बनी हुई है। खिसक लेना। मैंने वैसा ही किया। बाहर खानसामा मेरा सामान लिये खड़ा था। मैंने सामान लिया और चल दिया शहर की तरफ। कोई मिल ही जायेगा, जो कुछ दिन पनाह दे देगा, अनिश्चय में जी लेना मुझे तभी आ गया था।
पहले दिन जब बाकायदा ‘मास्साब’ बने तो बहुत अच्छा लगा। पहली तनख्वाह मिली ही थी कि पिताजी की मृत्य की खबर आ गयी। माँ के बचे जेवर बेच कर पिता का श्राद्ध किया और अध्यापकी के भरोसे बड़ी जिम्मेदारियाँ लेकर जिन्दगी के सफर पर निकल पड़े।
उस अवस्था की इन गर्दिशों का जिक्र मैं आखिर क्यों इस विस्तार से कर गया ? गर्दिशें बाद में भी आयीं, अब भी आती हैं, आगे भी आयेंगी पर उस उम्र की गर्दिशों की अपनी अहमियत है। लेखक की मानसिकता और व्यक्तित्व-निर्माण से इनका गहरा सम्बन्ध है।
मैंने कहा है-मैं बहुत भावुक संवेदनशील और बेचैन तबीयत का आदमी हूँ। सामान्य स्वभाव का आदमी ठंडे-ठंडे जिम्मेदारियाँ भी निभा लेता रोते-गाते दुनिया से तालमेल भी बिठा लेता और एक व्यक्तित्वहीन नौकरीपेशा आदमी की तरह जिन्दगी साधारण सन्तोष से भी गुजार लेता।
मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ जिम्मेदारियाँ, दुखों की वैसी पृष्ठभूमि और अब चारों तरफ से दुनिया के हमले-इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल था अपने व्यक्तित्व और चेतना की रक्षा। तब सोचा भी नहीं था कि लेखक बनूँगा। पर मैं अपने विशिष्ट व्यक्तित्व की रक्षा तब भी करना चाहता था।
जिम्मेदारी को गैर-जिम्मेदारी की तरह निभाओ !
मैंने तय किया-परसाई, डरो किसी से मत। डरे कि मरे। सीने को ऊपर-ऊपर कड़ा कर लो। भीतर तुम जो भी हो, जिम्मेदारी को गैर-जिम्मेदारी के साथ निभाओ। जिम्मेदारी को अगर जिम्मेदारी के साथ निभाओगे तो नष्ट हो जाओगे। और अपने से बाहर निकल कर सब में मिल जाने से व्यक्तित्व और विशिष्टता की हानि नहीं होती। लाभ ही होता है। अपने से बाहर निकलो। देखो, समझो और हँसो !
मैं डरा नहीं। बेईमानी करने में भी नहीं डरा। लोगों से नहीं डरा, तो नौकरियाँ गयीं। लाभ गये, पद गये इनाम गये। गैर-जिम्मेदार इतना कि बहन की शादी करने जा रहा हूँ। रेल में जेब कट गयी मगर अगले स्टेशन पर पूड़ी-साग खा कर मजे में बैठा हूँ कि चिन्ता नहीं। कुछ हो ही जायेगा। और हो गया। मेहनत और परेशानी जरूर पड़ी। यों कि बेहद बिजली-पानी के बीच एक पुजारी के साथ बिजली की चमक से रास्ता खोजते हुए रात भर में अपनी बड़ी बहन के गाँव पहुँचना और कुछ घंटे रहकर फिर वापसी यात्रा। फिर दौड़-धूप ! मगर मदद आ गयी और शादी भी हो गयी।
इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच मेरे भीतर लेखक कैसे जन्मा, यह सोचता हूँ। पहले अपने दुखों के प्रति सम्मोहन था। अपने को दुखी मान कर और मनवा कर आदमी राहत भी पा लेता है। बहुत लोग अपने लिए बेचारा सुनकर सन्तोष का अनुभव करते हैं। मुझे भी पहले ऐसा लगा। पर मैंने देखा, इतने ज्यादा बेचारों में मैं क्या बेचारा ! इतने विकट संघर्षों में मेरा क्या संघर्ष।
मेरा अनुमान है मैंने लेखन को दुनिया से लड़ने के लिए एक हथियार के रूप में अपनाया होगा। दूसरे, इसी में मैंने अपने व्यक्तित्व की रक्षा का रास्ता देखा। तीसरे, अपने को अविशिष्ट होने से बचाने के लिए मैंने लिखना शुरू कर दिया। यह तब की बात है, मेरा खयाल है, तब ऐसी ही बात होगी।
पर जल्दी ही मैं व्यक्तिगत दुःख के इस सम्मोहन जाल से निकल गया। मैंने अपने को विस्तार दे दिया। दुखी और भी हैं। अन्याय-पीड़ित और भी हैं। अनगिनत शोषित हैं। मैं उनमें से एक हूँ। पर मेरे हाथ में कलम है और मैं चेतना-सम्पन्न हूँ।
यहीं कहीं व्यंग्य लेखक का जन्म हुआ। मैंने सोचा होगा रोना नहीं है लड़ना है। जो हथियार हाथ में है, उसी से लड़ना है। मैंने तब ढंग से इतिहास, समाज, राजनीति और संस्कृति का अध्ययन शुरू किया। साथ ही एक औघड़ व्यक्तित्व बनाया। और बहुत गम्भीरता से व्यंग्य शुरू कर दिया।
मुक्ति अकेले की नहीं होती। अलग से अपना भला नहीं हो सकता। मनुष्ट की छटपटाहट है मुक्ति के लिए, सुख के लिए, न्याय के लिए। पर यह बड़ी लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती है। अकेले वही सुखी है, जिन्हें कोई लड़ाई नहीं लड़नी। उनकी बात अलग है। अनगिनत लोगों को सुखी देखता हूँ और अचरज करता हूँ कि ये सुखी कैसे हैं ! न उनके मन में सवाल उठते, न शंका उठती है। ये जब तब सिर्फ शिकायत कर लेते हैं। शिकायत भी सुख देती है। और वे ज्यादा सुखी हो जाते हैं। कबीर ने कहा है-
नौकरी मिली जबलपुर के सरकारी स्कूल में। किराये तक के पैसे नहीं। अध्यापक महोदय ने दरी में कपड़े बाँधे और बिना टिकट चढ़ गये गाड़ी में। सामान के कारण इस बार थोड़ा खटका था। पास में कलेक्टर का खानसामा बैठा था। बातचीत चलने लगी। आदमी मुझे अच्छा लगा। जबलपुर आने लगा तो मैंने उसे अपनी समस्या बतायी। उसने कहा-चिन्ता मत करो। सामान मुझे दो। मैं बाहर राह देखूँगा। तुम कहीं पानी पीने के बहाने सींखचों के पास पहुँच जाना। नल सींखचों के पास ही हैं। वहाँ सींखचों को उखाड़ कर निकलने की जगह बनी हुई है। खिसक लेना। मैंने वैसा ही किया। बाहर खानसामा मेरा सामान लिये खड़ा था। मैंने सामान लिया और चल दिया शहर की तरफ। कोई मिल ही जायेगा, जो कुछ दिन पनाह दे देगा, अनिश्चय में जी लेना मुझे तभी आ गया था।
पहले दिन जब बाकायदा ‘मास्साब’ बने तो बहुत अच्छा लगा। पहली तनख्वाह मिली ही थी कि पिताजी की मृत्य की खबर आ गयी। माँ के बचे जेवर बेच कर पिता का श्राद्ध किया और अध्यापकी के भरोसे बड़ी जिम्मेदारियाँ लेकर जिन्दगी के सफर पर निकल पड़े।
उस अवस्था की इन गर्दिशों का जिक्र मैं आखिर क्यों इस विस्तार से कर गया ? गर्दिशें बाद में भी आयीं, अब भी आती हैं, आगे भी आयेंगी पर उस उम्र की गर्दिशों की अपनी अहमियत है। लेखक की मानसिकता और व्यक्तित्व-निर्माण से इनका गहरा सम्बन्ध है।
मैंने कहा है-मैं बहुत भावुक संवेदनशील और बेचैन तबीयत का आदमी हूँ। सामान्य स्वभाव का आदमी ठंडे-ठंडे जिम्मेदारियाँ भी निभा लेता रोते-गाते दुनिया से तालमेल भी बिठा लेता और एक व्यक्तित्वहीन नौकरीपेशा आदमी की तरह जिन्दगी साधारण सन्तोष से भी गुजार लेता।
मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ जिम्मेदारियाँ, दुखों की वैसी पृष्ठभूमि और अब चारों तरफ से दुनिया के हमले-इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल था अपने व्यक्तित्व और चेतना की रक्षा। तब सोचा भी नहीं था कि लेखक बनूँगा। पर मैं अपने विशिष्ट व्यक्तित्व की रक्षा तब भी करना चाहता था।
जिम्मेदारी को गैर-जिम्मेदारी की तरह निभाओ !
मैंने तय किया-परसाई, डरो किसी से मत। डरे कि मरे। सीने को ऊपर-ऊपर कड़ा कर लो। भीतर तुम जो भी हो, जिम्मेदारी को गैर-जिम्मेदारी के साथ निभाओ। जिम्मेदारी को अगर जिम्मेदारी के साथ निभाओगे तो नष्ट हो जाओगे। और अपने से बाहर निकल कर सब में मिल जाने से व्यक्तित्व और विशिष्टता की हानि नहीं होती। लाभ ही होता है। अपने से बाहर निकलो। देखो, समझो और हँसो !
मैं डरा नहीं। बेईमानी करने में भी नहीं डरा। लोगों से नहीं डरा, तो नौकरियाँ गयीं। लाभ गये, पद गये इनाम गये। गैर-जिम्मेदार इतना कि बहन की शादी करने जा रहा हूँ। रेल में जेब कट गयी मगर अगले स्टेशन पर पूड़ी-साग खा कर मजे में बैठा हूँ कि चिन्ता नहीं। कुछ हो ही जायेगा। और हो गया। मेहनत और परेशानी जरूर पड़ी। यों कि बेहद बिजली-पानी के बीच एक पुजारी के साथ बिजली की चमक से रास्ता खोजते हुए रात भर में अपनी बड़ी बहन के गाँव पहुँचना और कुछ घंटे रहकर फिर वापसी यात्रा। फिर दौड़-धूप ! मगर मदद आ गयी और शादी भी हो गयी।
इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच मेरे भीतर लेखक कैसे जन्मा, यह सोचता हूँ। पहले अपने दुखों के प्रति सम्मोहन था। अपने को दुखी मान कर और मनवा कर आदमी राहत भी पा लेता है। बहुत लोग अपने लिए बेचारा सुनकर सन्तोष का अनुभव करते हैं। मुझे भी पहले ऐसा लगा। पर मैंने देखा, इतने ज्यादा बेचारों में मैं क्या बेचारा ! इतने विकट संघर्षों में मेरा क्या संघर्ष।
मेरा अनुमान है मैंने लेखन को दुनिया से लड़ने के लिए एक हथियार के रूप में अपनाया होगा। दूसरे, इसी में मैंने अपने व्यक्तित्व की रक्षा का रास्ता देखा। तीसरे, अपने को अविशिष्ट होने से बचाने के लिए मैंने लिखना शुरू कर दिया। यह तब की बात है, मेरा खयाल है, तब ऐसी ही बात होगी।
पर जल्दी ही मैं व्यक्तिगत दुःख के इस सम्मोहन जाल से निकल गया। मैंने अपने को विस्तार दे दिया। दुखी और भी हैं। अन्याय-पीड़ित और भी हैं। अनगिनत शोषित हैं। मैं उनमें से एक हूँ। पर मेरे हाथ में कलम है और मैं चेतना-सम्पन्न हूँ।
यहीं कहीं व्यंग्य लेखक का जन्म हुआ। मैंने सोचा होगा रोना नहीं है लड़ना है। जो हथियार हाथ में है, उसी से लड़ना है। मैंने तब ढंग से इतिहास, समाज, राजनीति और संस्कृति का अध्ययन शुरू किया। साथ ही एक औघड़ व्यक्तित्व बनाया। और बहुत गम्भीरता से व्यंग्य शुरू कर दिया।
मुक्ति अकेले की नहीं होती। अलग से अपना भला नहीं हो सकता। मनुष्ट की छटपटाहट है मुक्ति के लिए, सुख के लिए, न्याय के लिए। पर यह बड़ी लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती है। अकेले वही सुखी है, जिन्हें कोई लड़ाई नहीं लड़नी। उनकी बात अलग है। अनगिनत लोगों को सुखी देखता हूँ और अचरज करता हूँ कि ये सुखी कैसे हैं ! न उनके मन में सवाल उठते, न शंका उठती है। ये जब तब सिर्फ शिकायत कर लेते हैं। शिकायत भी सुख देती है। और वे ज्यादा सुखी हो जाते हैं। कबीर ने कहा है-
सुखिया सब संसार है, खावै और सोवै।
दुखिया दास कबीर है, जागै और रोवै।
दुखिया दास कबीर है, जागै और रोवै।
जागने वाले का रोना कभी खत्म नहीं होता। व्यंग्य लेखक की गर्दिश भी खत्म नहीं होगी।
ताजा गर्दिश यह है कि पिछले दिनों राजनीतिक पद के लिए पापड़ बेलते रहे। कहीं से उम्मीद दिला दी गयी कि राज्य सभा में हो जायेगा। एक महीना बड़ी गर्दिश में बीता। घुसपैठ की आदत नहीं है चिट भीतर भेज कर बाहर बैठे रहने में हर क्षण मृत्यु पीड़ा होती है। बहादुर लोग तो महीनों चिट भेज कर बाहर बैठे रहते हैं, मगर मरते नहीं। अपने से नहीं बनता। पिछले कुछ महीने ऐसी गर्दिश के थे। कोई लाभ खुद चल कर दरवाजे पर नहीं आता। उसे मनाना पड़ता है। चिरौरी करनी पड़ती है। लाभ थूकता है तो उसे हथेली पर लेना पड़ता है। इस कोशिश में बड़ी तकलीफ हुई। बड़ी गर्दिश भोगी।
मेरे जैसे लेखक की एक और गर्दिश है। भीतर जितना बवंडर महसूस कर रहे हैं, उतना शब्दों में नहीं आ रहा है, तो रात-दिन बेचैन हैं। यह बड़ी गर्दिस का वक्त होता है जिसे सर्जक ही समझ सकता है।
यों गर्दिशों की एक याद है। पर सही बात यह है कि कोई दिन गर्दिश से खाली नहीं है। और न कभी गर्दिश का अन्त होना है। यह और बात है कि शोभा के लिए कुछ अच्छे किस्म की गर्दिश चुन ली जायें। उनका मेकअप कर दिया जाये, उन्हें अदाएँ सिखा दी जायें-थोड़ी चुलबुली गर्दिश हो तो और अच्छा-और पाठक से कहा जाये-ले भाई, देख मेरी गर्दिश !
ताजा गर्दिश यह है कि पिछले दिनों राजनीतिक पद के लिए पापड़ बेलते रहे। कहीं से उम्मीद दिला दी गयी कि राज्य सभा में हो जायेगा। एक महीना बड़ी गर्दिश में बीता। घुसपैठ की आदत नहीं है चिट भीतर भेज कर बाहर बैठे रहने में हर क्षण मृत्यु पीड़ा होती है। बहादुर लोग तो महीनों चिट भेज कर बाहर बैठे रहते हैं, मगर मरते नहीं। अपने से नहीं बनता। पिछले कुछ महीने ऐसी गर्दिश के थे। कोई लाभ खुद चल कर दरवाजे पर नहीं आता। उसे मनाना पड़ता है। चिरौरी करनी पड़ती है। लाभ थूकता है तो उसे हथेली पर लेना पड़ता है। इस कोशिश में बड़ी तकलीफ हुई। बड़ी गर्दिश भोगी।
मेरे जैसे लेखक की एक और गर्दिश है। भीतर जितना बवंडर महसूस कर रहे हैं, उतना शब्दों में नहीं आ रहा है, तो रात-दिन बेचैन हैं। यह बड़ी गर्दिस का वक्त होता है जिसे सर्जक ही समझ सकता है।
यों गर्दिशों की एक याद है। पर सही बात यह है कि कोई दिन गर्दिश से खाली नहीं है। और न कभी गर्दिश का अन्त होना है। यह और बात है कि शोभा के लिए कुछ अच्छे किस्म की गर्दिश चुन ली जायें। उनका मेकअप कर दिया जाये, उन्हें अदाएँ सिखा दी जायें-थोड़ी चुलबुली गर्दिश हो तो और अच्छा-और पाठक से कहा जाये-ले भाई, देख मेरी गर्दिश !
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book