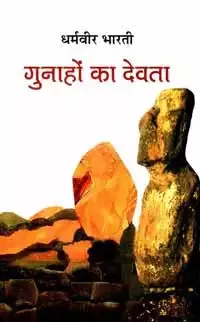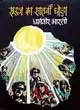|
लेख-निबंध >> शब्दिता शब्दिताधर्मवीर भारती
|
369 पाठक हैं |
||||||
रचनात्मक वैविध्य और जीवन के प्रति लेखक के गहन संवेदात्मक राग का वर्णन है...
Shabdita
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
भाषा, साहित्य, संस्कृति और इतिहास के किसी भी जागरुक रचनाकार की संवेदात्मक रचनाशीलता के अभिन्न अंग होते हैं। डॉ. धर्मवीर भारती हिन्दी के यशस्वी कवि, कथाकार और सुधी सम्पादक के रूप में सुपरिचित हैं। ‘कनुप्रिया’, ‘अंधायुग’, और ‘सूरज का सातवाँ घोड़ा’ जैसी रचनाएँ समकालीन हिंदी साहित्य में अपना ऐतिहासिक महत्त्व रखती हैं।
‘शब्दिता’ भारत जी के निबन्धों का संग्रह है। इनमें कुछ तो ‘धर्मयुग’ के ‘शब्दिता’ शीर्षक बहुचर्चित स्तम्भ से संग्रहित हैं, और कुछ अन्य पत्र-पत्रिकाओं से लिये गये हैं। स्वभावता इन निबन्धों में से प्रायः प्रत्येक का एक समय संदर्भ है, लेकिन लेखकीय दृष्टि उससे सम्बद्ध समस्या अथवा विचारणीय मुद्दे को उसकी समग्रता में देखती है। उसकी पृष्ठभूमि में भारतीय संस्कृति की जो प्रवहमान परम्परा है, लेखक उसे कहीं भी आंख-ओझल नहीं करता। भारतीय समाज की विभिन्न समस्याओं, उसकी संरचनात्मक जटिलताओं और विश्वजनीन वैचारिक वादों-प्रतिवादों पर भी लेखक ने अपनी बेबाक राय प्रकट की है, फिर चाहे हिंदी उर्दू का मसला हो, अंग्रेजी के वर्चस्व का सवाल हो, या फिर साम्यवादी व्यवस्था के अपने ही अंतर्विरोधों के चलते ध्वस्त हो जाने का अभूतपूर्व घटनाक्रम।
इस सबके अतिरिक्त रचनात्मक वैविध्य और जीवन के प्रति गहन संवेदात्मक राग के लिए भी उल्लेखनीय हैं। अनेक निबंधों में भारती जी अपने समकालीनों और प्रियजनों को तो याद करते ही हैं, मॉरिशस और इंडोनेशिया जैसे एशियाई देशों में गंगा-यमुना के सामाजिक-सांस्कृतिक महत्त्व का भी ह्रदयग्राही शब्दचित्र उकेरते हैं। कहना न होना कि यह निबंधकृति पाठकों को विभिन्न विचार-वीथियों के सहारे एक सांस्कृतिक यात्रा कराने में सक्षम हैं।
इस अश्रबिन्दु की तरलाई को वही महसूस कर सकता है, जिसमें, इस समवेत पीड़ा की संवेदना की गहराई में उतर कर महसूस करने की क्षमता हो। पर जो क्षेत्रगत, सम्प्रदायगत, भाषागत या दलगत राजनीति की आँच में हाथ सेंक कर अपने लिए सुविधाएँ और नामवरी हासिल करने की जुगाड़ में ही लगे रहते हैं, ऐसे लोग उनका दर्द कैसे समझ पाएँगे, जिन्हें सचमुच आग पर पाँव रख कर चलना होता है ? और सांस्कृतिक समन्वयों की नींव तो उसी दर्द पर रखी जाती रही है।
‘शब्दिता’ भारत जी के निबन्धों का संग्रह है। इनमें कुछ तो ‘धर्मयुग’ के ‘शब्दिता’ शीर्षक बहुचर्चित स्तम्भ से संग्रहित हैं, और कुछ अन्य पत्र-पत्रिकाओं से लिये गये हैं। स्वभावता इन निबन्धों में से प्रायः प्रत्येक का एक समय संदर्भ है, लेकिन लेखकीय दृष्टि उससे सम्बद्ध समस्या अथवा विचारणीय मुद्दे को उसकी समग्रता में देखती है। उसकी पृष्ठभूमि में भारतीय संस्कृति की जो प्रवहमान परम्परा है, लेखक उसे कहीं भी आंख-ओझल नहीं करता। भारतीय समाज की विभिन्न समस्याओं, उसकी संरचनात्मक जटिलताओं और विश्वजनीन वैचारिक वादों-प्रतिवादों पर भी लेखक ने अपनी बेबाक राय प्रकट की है, फिर चाहे हिंदी उर्दू का मसला हो, अंग्रेजी के वर्चस्व का सवाल हो, या फिर साम्यवादी व्यवस्था के अपने ही अंतर्विरोधों के चलते ध्वस्त हो जाने का अभूतपूर्व घटनाक्रम।
इस सबके अतिरिक्त रचनात्मक वैविध्य और जीवन के प्रति गहन संवेदात्मक राग के लिए भी उल्लेखनीय हैं। अनेक निबंधों में भारती जी अपने समकालीनों और प्रियजनों को तो याद करते ही हैं, मॉरिशस और इंडोनेशिया जैसे एशियाई देशों में गंगा-यमुना के सामाजिक-सांस्कृतिक महत्त्व का भी ह्रदयग्राही शब्दचित्र उकेरते हैं। कहना न होना कि यह निबंधकृति पाठकों को विभिन्न विचार-वीथियों के सहारे एक सांस्कृतिक यात्रा कराने में सक्षम हैं।
इस अश्रबिन्दु की तरलाई को वही महसूस कर सकता है, जिसमें, इस समवेत पीड़ा की संवेदना की गहराई में उतर कर महसूस करने की क्षमता हो। पर जो क्षेत्रगत, सम्प्रदायगत, भाषागत या दलगत राजनीति की आँच में हाथ सेंक कर अपने लिए सुविधाएँ और नामवरी हासिल करने की जुगाड़ में ही लगे रहते हैं, ऐसे लोग उनका दर्द कैसे समझ पाएँगे, जिन्हें सचमुच आग पर पाँव रख कर चलना होता है ? और सांस्कृतिक समन्वयों की नींव तो उसी दर्द पर रखी जाती रही है।
गुमशुदा हिन्दीपन की तलाश
पिछला वर्ष सन् ’89 कितना चुपचाप बीत गया। अब तो ’90 को लगे भी महीना होने को आया है। हम इस बीच भूल भी चुके हैं कि पिछला वर्ष हिन्दी के तीन दिग्गज कवियों की जन्म शताब्दी का वर्ष था। मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और माखनलाल चतुर्वेदी। वर्ष के प्रारम्भ में कुछ उत्सव, समारोह हुए। पत्र-पत्रिकाओं में कुछ लेख-वेख छप-छपा गये बस ! जिन महाकवियों ने अपना पूरा जीवन हमारे साहित्य को समृद्ध बनाने में अर्पित कर दिया, यदि और नहीं तो पाठ्यक्रमों में जिनकी रचनाएँ पढ़-पढ़ कर हिन्दी भाषियों की कम से कम पाँच-छह पीढ़ियाँ जवान हुई हों उनकी जन्म शताब्दी का वर्ष ऐसा सुनसान बीत जाये यह कुछ अजीब-सा नहीं लगता ? आखिर हिन्दी भाषी अपने साहित्यकों, अपनी भाषा और अपनी विरासत के प्रति इतने उदास क्यों हो चुके हैं ?
एक बात यह कही जा सकती है कि कविता खुद जीवन से इतनी कट चुकी है कि कोई उसकी परवाह क्यों करे ? हो सकता है कि कुछ आधुनिक काव्यधाराओं के बारे में यह बात सच हो पर मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और माखनलाल जी के बारे में हैं जो चाहे या अनचाहे हर संवेदनशील हिन्दी पाठक को कभी-न-कभी, किसी-न-किसी रचना द्वारा आलोडित कर चुके हैं।
और केवल कविता की बात नहीं है। अपनी पूरी सांस्कृतिक विरासत के प्रति हिन्दी भाषी उस तरह सचेत नहीं हैं जैसा बंगला, गुजराती, कन्नड़ या तमिल-भाषी हैं। बल्कि सच तो यह है कि महाराष्ट्र से लेकर केरल तक हिन्दी से जुड़े हुए जो अहिन्दी-भाषी विद्वान तथा रंगकर्मी हैं वे हिन्दी साहित्य और संस्कृति के प्रति अधिक जागरूक हैं।
कई बार मन कचोट उठता है। पिछले लगभग पचीस वर्षों से देख रहा हूँ कि किस प्रकार सत्यदेव दुबे ने अकेले दम संघर्ष करके हिन्दी के रंगमंच को बम्बई जैसे स्थान में प्रतिष्ठित कराया। लेकिन जब भी उनके नाटक देखने गया। तो पाया कि गिने-चुने हिन्दी बुद्धिजीवियों के अलावा वहाँ न तो हिन्दीभाषी सामान्य-जन हैं, न हिन्दीभाषी वरिष्ठ लेखक-पत्रकार हैं, और हिन्दी अध्यापक तो हैं ही नहीं, मराठी-भाषी, गुजरातीभाषी, कन्नड़भाषी दर्शक बहुतायत में हैं। यहाँ तक कि हिन्दी की गतिविधियों को बहुधा उपेक्षा से देखनेवाले अंग्रेजी पत्रकार और रंग समीक्षक भी मिल जायेंगे और अच्छा प्रदर्शन होने पर प्रशंसा भी करेंगे, पर हिन्दी ? बम्बई के एक महत्त्वपूर्ण दैनिक हिन्दी पत्र ने तो वर्षों तक दुबे का बहिष्कार कर रखा था। क्यों ? यह तो उनके तत्कालीन सम्पादक ही जानें।
मीडिया के किसी पक्ष को लीजिए। मण्डी हाउस के इर्दगिर्द हिन्दी में सीरियल बनाने वालों की भीड़ जमा रहती है। उनका हिन्दी से कितना सरोकार है ? आखिर गुलज़ार ने ग़ालिब के जीवन पर इतना प्रभावशाली सीरियल बनाया पर किसी हिन्दी वाले को यह नहीं सूझा कि भारतेन्दु हरिश्चनद्र के घटनापूर्ण, मार्मिक और अर्थभरे जीवन पर सीरियल बन सकता है। हिन्दी की साहित्यिक कृतियाँ ? एक-दो दूरदर्शन पर आयीं भी तो कैसे अजीब रूप में, ‘राग दरबारी’ की पहली प्रस्तुति वह प्रभाव ही नहीं दे पायी जो मूल कृति में है, ‘कब तक पुकारूँ’ की पहली किस्त देखी। नटों से लोकभाषा बुलवाई गयी है मगर नटों-बनजारों की लोकभाषा में अवधी ? चकित रह गया मैं, क्या पूरी टीम में कोई ऐसा नहीं था जो भरतपुर के ग्रामीण अंचल में जाकर उस राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा के मीठे रूप को डायलाग में गूँथ सकता, जो वहाँ के नट-बनजारे बोलते हैं। लिखित हिन्दी तो समृद्ध है ही पर बोली जाने वाली हिन्दी के कितने रूप हैं और हरेक अपने में कितना समृद्ध। पर दूरदर्शन, फिल्म या रेड़ियो में कभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। पात्र देहाती हैं तो उससे आधी-अधूरी अवधी बुलवा दो क्योंकि शरू-शुरू में कलकत्ते के न्यू थियेर्टस की फिल्मों में देहाती पुरबिया पात्र अवधी बोलते थे। अभी कुछ वर्ष पहले एक फिल्म देखी थी। गोआ और कोंकणी अंचल की एक प्रेम कहानी थी। नौ गजी साड़ियाँ आकर्षक रूप में लपेटे गोआ की मछेरिनें गलत-सलत उच्चारण में धारा-प्रावह अवधी बोल रही थीं। उस क्षेत्र में जाइए। वहाँ के लोग कोंकणी, मराठी मिश्रित हिन्दी बोलते हैं उसका एक अलग ही स्वाद है। पर उसे संवादों में उतारने की मेहनत कौन करे ?
पता नहीं कब तक यह हालत चलेगी ? हिन्दीभाषियों में खुद जब तक अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति चेतना नहीं जागेगी तब तक हालात सुधरना असंभव है।
क्या सदा से हिन्दीभाषी लोग इस तरह साहित्य-चेतना से कट रहे हैं ? शायद नहीं, मुझे याद है, मैं स्कूल में पढ़ता था। उस समय इलाहाबाद के अग्रवाल स्कूल में एक मेला आयोजित किया गया था ‘महावीर मेला’। या तो श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी की षष्टिपूर्ति थी या सरस्वती के सम्पादन के 25 वर्ष पूरे हुए थे, असर क्या था, यह याद नहीं पर उस मेले की धुँधली-सी याद है। न केवल इंडियन प्रेस वरन् इलाहाबाद के कई प्रकाशकों की दुकानें थीं, किताबों की खरीद पर विशेष कमीशन घोषित किया गया था, सूचीपत्र बाँटे जा रहे थे, चाट के खोमचे और पान वालों की दुकानें भी थीं। मेला शायद तीन दिन चला था। इलाहाबद में जितने कॉलेज थे उन्होंने हिन्दी विषय लेने वाले छात्रों को अध्यापकों के साथ बारी-बारी से मेले में भेजा था। बहुत पहले की बात है और बहुत धुँधली याद है। अत: यह याद नहीं कि अन्य क्या कार्यक्रम हुए। सच पूछिए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन हैं और उनका क्या महत्त्व है, यह मुझे उस समय ज्ञात ही नहीं था। पर इतना याद है कि उस समय पढ़े-लिखे लोग कम थे, लेकिन जो थे उनमें एक चेतना थी। मैथिली शरण गुप्त की भारत-भारती में दिये गये तथ्यों पर बहसें होती थीं और लोग अक्सर दोहराते थे भारत-भारती की ये आरम्भिक पंक्तियाँ :
एक बात यह कही जा सकती है कि कविता खुद जीवन से इतनी कट चुकी है कि कोई उसकी परवाह क्यों करे ? हो सकता है कि कुछ आधुनिक काव्यधाराओं के बारे में यह बात सच हो पर मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और माखनलाल जी के बारे में हैं जो चाहे या अनचाहे हर संवेदनशील हिन्दी पाठक को कभी-न-कभी, किसी-न-किसी रचना द्वारा आलोडित कर चुके हैं।
और केवल कविता की बात नहीं है। अपनी पूरी सांस्कृतिक विरासत के प्रति हिन्दी भाषी उस तरह सचेत नहीं हैं जैसा बंगला, गुजराती, कन्नड़ या तमिल-भाषी हैं। बल्कि सच तो यह है कि महाराष्ट्र से लेकर केरल तक हिन्दी से जुड़े हुए जो अहिन्दी-भाषी विद्वान तथा रंगकर्मी हैं वे हिन्दी साहित्य और संस्कृति के प्रति अधिक जागरूक हैं।
कई बार मन कचोट उठता है। पिछले लगभग पचीस वर्षों से देख रहा हूँ कि किस प्रकार सत्यदेव दुबे ने अकेले दम संघर्ष करके हिन्दी के रंगमंच को बम्बई जैसे स्थान में प्रतिष्ठित कराया। लेकिन जब भी उनके नाटक देखने गया। तो पाया कि गिने-चुने हिन्दी बुद्धिजीवियों के अलावा वहाँ न तो हिन्दीभाषी सामान्य-जन हैं, न हिन्दीभाषी वरिष्ठ लेखक-पत्रकार हैं, और हिन्दी अध्यापक तो हैं ही नहीं, मराठी-भाषी, गुजरातीभाषी, कन्नड़भाषी दर्शक बहुतायत में हैं। यहाँ तक कि हिन्दी की गतिविधियों को बहुधा उपेक्षा से देखनेवाले अंग्रेजी पत्रकार और रंग समीक्षक भी मिल जायेंगे और अच्छा प्रदर्शन होने पर प्रशंसा भी करेंगे, पर हिन्दी ? बम्बई के एक महत्त्वपूर्ण दैनिक हिन्दी पत्र ने तो वर्षों तक दुबे का बहिष्कार कर रखा था। क्यों ? यह तो उनके तत्कालीन सम्पादक ही जानें।
मीडिया के किसी पक्ष को लीजिए। मण्डी हाउस के इर्दगिर्द हिन्दी में सीरियल बनाने वालों की भीड़ जमा रहती है। उनका हिन्दी से कितना सरोकार है ? आखिर गुलज़ार ने ग़ालिब के जीवन पर इतना प्रभावशाली सीरियल बनाया पर किसी हिन्दी वाले को यह नहीं सूझा कि भारतेन्दु हरिश्चनद्र के घटनापूर्ण, मार्मिक और अर्थभरे जीवन पर सीरियल बन सकता है। हिन्दी की साहित्यिक कृतियाँ ? एक-दो दूरदर्शन पर आयीं भी तो कैसे अजीब रूप में, ‘राग दरबारी’ की पहली प्रस्तुति वह प्रभाव ही नहीं दे पायी जो मूल कृति में है, ‘कब तक पुकारूँ’ की पहली किस्त देखी। नटों से लोकभाषा बुलवाई गयी है मगर नटों-बनजारों की लोकभाषा में अवधी ? चकित रह गया मैं, क्या पूरी टीम में कोई ऐसा नहीं था जो भरतपुर के ग्रामीण अंचल में जाकर उस राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा के मीठे रूप को डायलाग में गूँथ सकता, जो वहाँ के नट-बनजारे बोलते हैं। लिखित हिन्दी तो समृद्ध है ही पर बोली जाने वाली हिन्दी के कितने रूप हैं और हरेक अपने में कितना समृद्ध। पर दूरदर्शन, फिल्म या रेड़ियो में कभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। पात्र देहाती हैं तो उससे आधी-अधूरी अवधी बुलवा दो क्योंकि शरू-शुरू में कलकत्ते के न्यू थियेर्टस की फिल्मों में देहाती पुरबिया पात्र अवधी बोलते थे। अभी कुछ वर्ष पहले एक फिल्म देखी थी। गोआ और कोंकणी अंचल की एक प्रेम कहानी थी। नौ गजी साड़ियाँ आकर्षक रूप में लपेटे गोआ की मछेरिनें गलत-सलत उच्चारण में धारा-प्रावह अवधी बोल रही थीं। उस क्षेत्र में जाइए। वहाँ के लोग कोंकणी, मराठी मिश्रित हिन्दी बोलते हैं उसका एक अलग ही स्वाद है। पर उसे संवादों में उतारने की मेहनत कौन करे ?
पता नहीं कब तक यह हालत चलेगी ? हिन्दीभाषियों में खुद जब तक अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति चेतना नहीं जागेगी तब तक हालात सुधरना असंभव है।
क्या सदा से हिन्दीभाषी लोग इस तरह साहित्य-चेतना से कट रहे हैं ? शायद नहीं, मुझे याद है, मैं स्कूल में पढ़ता था। उस समय इलाहाबाद के अग्रवाल स्कूल में एक मेला आयोजित किया गया था ‘महावीर मेला’। या तो श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी की षष्टिपूर्ति थी या सरस्वती के सम्पादन के 25 वर्ष पूरे हुए थे, असर क्या था, यह याद नहीं पर उस मेले की धुँधली-सी याद है। न केवल इंडियन प्रेस वरन् इलाहाबाद के कई प्रकाशकों की दुकानें थीं, किताबों की खरीद पर विशेष कमीशन घोषित किया गया था, सूचीपत्र बाँटे जा रहे थे, चाट के खोमचे और पान वालों की दुकानें भी थीं। मेला शायद तीन दिन चला था। इलाहाबद में जितने कॉलेज थे उन्होंने हिन्दी विषय लेने वाले छात्रों को अध्यापकों के साथ बारी-बारी से मेले में भेजा था। बहुत पहले की बात है और बहुत धुँधली याद है। अत: यह याद नहीं कि अन्य क्या कार्यक्रम हुए। सच पूछिए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन हैं और उनका क्या महत्त्व है, यह मुझे उस समय ज्ञात ही नहीं था। पर इतना याद है कि उस समय पढ़े-लिखे लोग कम थे, लेकिन जो थे उनमें एक चेतना थी। मैथिली शरण गुप्त की भारत-भारती में दिये गये तथ्यों पर बहसें होती थीं और लोग अक्सर दोहराते थे भारत-भारती की ये आरम्भिक पंक्तियाँ :
हम कौन थे क्या हो गये हैं और क्या होंगे अभी
आओ विचारें आज मिल कर ये समस्याएँ सभी,
आओ विचारें आज मिल कर ये समस्याएँ सभी,
लगता है एक बार फिर हिन्दीभाषियों को विचारना होगा कि ‘वे कौन थे, क्या हो गये हैं।’ वरना गिरावट का यह क्रम रुकेगा नहीं !
ऊलजलूल के भी अर्थ हैं
‘ऊलजलूल का नाटक’। आपने कभी यह वाक्यांश पढ़ा है ? अब तो कोई उसकी बात नहीं करता। लेकिन आज से कई दशक पहले हिन्दी समीक्षा में यह शब्द बहुधा इस्तेमाल होता था और सीधा अनुवाद था अ
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book