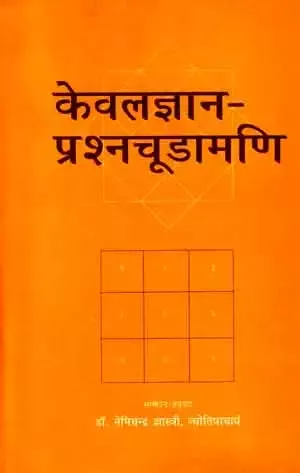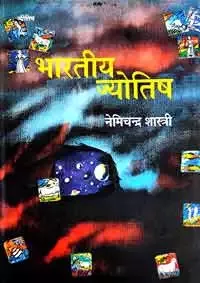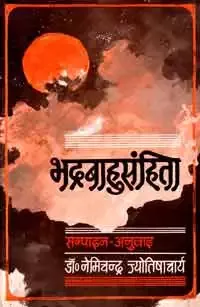|
वास्तु एवं ज्योतिष >> केवलज्ञान प्रश्नचूड़ामणि केवलज्ञान प्रश्नचूड़ामणिनेमिचन्द्र शास्त्री
|
267 पाठक हैं |
|||||||
किसी भी फल, फूल, देवता, नदी, या पहाड़ का नाम लो और मनचाही बात बूझो...
kevalgyan- prashnachudamani
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘केवलज्ञानप्रश्नचूडामणि’-अर्थात किसी भी फल, फूल, देवता, नदी, या पहाड़ का नाम लो और मनचाही बात बूझो। जीवन, मरण, लाभ, हानि, संयोग, वियोग, सुख-दुःख, चोरी गयी वस्तु का पता, परदेशी के लौटने का समय, पुत्र या कन्या प्राप्ति, मुकदमा जीतने हारने की बात, जो कुछ भी चाहे पूछों और उत्तर अपने आप प्राप्त करें।
‘केवलज्ञानप्रश्नचूड़ामणि’ प्रश्नशास्त्र का एक लघुकाय किन्तु महत्त्वपूर्ण व चमत्कारी ग्रंथ है। प्रश्नशास्त्र फलित ज्योतिष का अंग जाना जाता है। इसमें प्रश्नकर्ता के प्रश्नानुसार बिना जन्म कुण्डली के फल बताया जाता है। ज्योतिशास्त्र में प्रश्नों के उत्तर तीन प्रकार से दिये जाते हैः प्रश्न काल मे जानकर, स्वर के आधार पर प्रश्नाक्षरों के आधार पर। इन तीनों सिद्धान्तों में अधिक मनोवैज्ञानिक एवं प्रामाणिक है। प्रस्तुत कृति में एक सिद्धान्त का अत्यन्त सरल एवं विशद विवेचन है।
प्रश्नकर्ता के प्रश्ननुसार अक्षरों से अथवा पाँच वर्गों के अक्षर स्थापित करके स्पर्श कराकर प्रश्नों का फल किसी प्रकार ज्ञात किया जाता है, इसका विवेचन किया गया है। विद्वान सम्पादक ने विस्तृत प्रस्तावना तथा विभिन्न परिशिष्टों द्वारा को और अधिक उपयोगी बना दिया है। प्रस्तुत कृति का यह नवीन संस्करण इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पाठकों के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है।
‘केवलज्ञानप्रश्नचूड़ामणि’ प्रश्नशास्त्र का एक लघुकाय किन्तु महत्त्वपूर्ण व चमत्कारी ग्रंथ है। प्रश्नशास्त्र फलित ज्योतिष का अंग जाना जाता है। इसमें प्रश्नकर्ता के प्रश्नानुसार बिना जन्म कुण्डली के फल बताया जाता है। ज्योतिशास्त्र में प्रश्नों के उत्तर तीन प्रकार से दिये जाते हैः प्रश्न काल मे जानकर, स्वर के आधार पर प्रश्नाक्षरों के आधार पर। इन तीनों सिद्धान्तों में अधिक मनोवैज्ञानिक एवं प्रामाणिक है। प्रस्तुत कृति में एक सिद्धान्त का अत्यन्त सरल एवं विशद विवेचन है।
प्रश्नकर्ता के प्रश्ननुसार अक्षरों से अथवा पाँच वर्गों के अक्षर स्थापित करके स्पर्श कराकर प्रश्नों का फल किसी प्रकार ज्ञात किया जाता है, इसका विवेचन किया गया है। विद्वान सम्पादक ने विस्तृत प्रस्तावना तथा विभिन्न परिशिष्टों द्वारा को और अधिक उपयोगी बना दिया है। प्रस्तुत कृति का यह नवीन संस्करण इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पाठकों के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है।
आदिवचन
(प्रथम संस्करण से)
अनन्त आकाश मण्डल में अपने प्रोज्ज्वल प्रकाश का प्रसार करते हुए असंख्य नक्षत्र-दीपों ने अपने किरण-करों के संकेत तथा अपनी लोकमयी मूकभाषा से मानव-मानस में अपने इतिवृत्त की जिज्ञासा जब जागरुक की थी, तब अनेक तपोधन महर्षियों ने उनके समस्त इतिवेद्यों की करामलक करने की तीव्र तपोमय दीर्घतम साधनाएँ की थीं और वे अपने योग-प्रभावप्राप्त दिव्य दृष्टियों से उनके रहस्यों का साक्षात्कार करने में समर्थ हुए थे। उन महामहिम महर्षियों के अन्तस्तल में अपार करुणा थी; अतः वे किसी भी वस्तु के ज्ञानोपन को पातक मानते थे। उन्होंने अपनी नक्षत्र सम्बन्धी ज्ञानरासि का जनहित की भावना से बहुत ही सुन्दर संकलन और संग्रन्थन कर दिया था। उनके इस संग्रथित-ज्ञानकोष की ही ज्योतिषशास्त्र के नाम से प्रसिद्धि हुई थी जो अब भी उसी रूप में है।
इस विषय में किसी को किंतिच भी विप्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए कि सर्वप्रथम ज्योतिषविद्या का ही प्रदुर्भाव हुआ था और वह भी भारतवर्ष में ही। बाद में इसी विद्या के प्रकाशन ने सारे भूमण्डल को आलोकित किया और अन्य अनेक विद्याओं को जन्म दिया। यह स्पष्ट है कि एक अंक का प्रकाश होने के बाद ही ‘एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’ इस अद्वैत सिद्धांत का अवतण हुआ था। दो संख्या का परिचय होने के बाद ही द्वैत विचार का उन्मेष हुआ। अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत तत्वों की संख्या में न्याय, वैशेषिक सांख्ययोग, पूर्व और उत्तर मीमांसा के विभिन्न मत में इन सब के जन्म की ज्योतिषविद्या की पाश्चाद्भाविता निर्विवाद रूप से सभी को मान्य है। पंचमहाभूत, शब्दाशास्त्र के चतुर्दश सूत्र तथा साहित्य के नवरस आदि की चर्चा, अंकभेदादि सम्बन्ध, गुरुलघ्वादि सम्बन्ध, छन्द की रचना आदि ने इस ज्योतिषशास्त्र से ही स्वरूपलाभ पाया है।
ऐसे ही ज्योतिषशास्त्र की प्राचीनता के परीक्षण में अन्य अनेक बातों को छोड़कर केवल ग्रहोच्च के ज्ञान से ही यदि वर्ष की गणना की जाय तो सूर्य की उच्च से गणना करने पर,
इस विषय में किसी को किंतिच भी विप्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए कि सर्वप्रथम ज्योतिषविद्या का ही प्रदुर्भाव हुआ था और वह भी भारतवर्ष में ही। बाद में इसी विद्या के प्रकाशन ने सारे भूमण्डल को आलोकित किया और अन्य अनेक विद्याओं को जन्म दिया। यह स्पष्ट है कि एक अंक का प्रकाश होने के बाद ही ‘एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’ इस अद्वैत सिद्धांत का अवतण हुआ था। दो संख्या का परिचय होने के बाद ही द्वैत विचार का उन्मेष हुआ। अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत तत्वों की संख्या में न्याय, वैशेषिक सांख्ययोग, पूर्व और उत्तर मीमांसा के विभिन्न मत में इन सब के जन्म की ज्योतिषविद्या की पाश्चाद्भाविता निर्विवाद रूप से सभी को मान्य है। पंचमहाभूत, शब्दाशास्त्र के चतुर्दश सूत्र तथा साहित्य के नवरस आदि की चर्चा, अंकभेदादि सम्बन्ध, गुरुलघ्वादि सम्बन्ध, छन्द की रचना आदि ने इस ज्योतिषशास्त्र से ही स्वरूपलाभ पाया है।
ऐसे ही ज्योतिषशास्त्र की प्राचीनता के परीक्षण में अन्य अनेक बातों को छोड़कर केवल ग्रहोच्च के ज्ञान से ही यदि वर्ष की गणना की जाय तो सूर्य की उच्च से गणना करने पर,
‘‘अजवृषभमृगाङ्गनाकुलीरा झषवणिजौ च दिवाकरादितुङ्गाः।
दशशिखिमनुयुक्तिथीन्द्रियांशैस्त्रिनवकविंशतिभिश्च तेस्तनीचाः।।’’
दशशिखिमनुयुक्तिथीन्द्रियांशैस्त्रिनवकविंशतिभिश्च तेस्तनीचाः।।’’
इस व्यवहारिक ज्योतिष-गणना के प्रयत्न की न्यूनतम सत्ता आज से 21,80,296 वर्ष पूर्व सिद्ध होती है। इस प्रकार मंगल के उच्च से विचार करने पर 1,12,29,390 वर्ष तथा शनैश्चर के उच्च से विचार करने पर 1,12,07,690 वर्ष पूर्व की जगत् में ज्योतिष के विकशित रूप में होने की सिद्धि होता है, जो आधुनिक संसार के लोगों के लिए, विशेषकर पाश्चात्य विज्ञानविशारदों के लिए बड़े आश्चर्य की सामग्री है।
‘‘ज्योतिषशास्त्रफलं पुराणगणकैरादेश इत्युच्यते...’’
आचार्यों के इस प्रकार के वचनों के अनुसार मानव-जगत में विविध आदेश करना ही इस अपूर्व अप्रतिम ज्योतिषशास्त्र का प्रधान लक्ष्य है।
इसी आदेश के एक अंग का नाम प्रश्नावगम तन्त्र है। इस प्रश्न-प्रणाली को जैन सिद्धान्त के प्रवर्तकों ने भी आवश्यक समझकर बड़ी तत्परता से अपनाया था और उसकी सारी विचारधाराएँ ‘केवलज्ञानप्रश्नचूडामणि’ के रूप में लेखबद्ध कर सुरक्षित रखी थीं, किन्तु वह ग्रन्थ अत्यन्त दुरुह होने के कारण सर्वसाधारण का उपकार करने में पूर्णरूपेण स्वयं समर्थ नहीं रहा। अतः मेरे योग्यतम शिष्य श्री नेमिचन्द्र जैन ने बहुत ही विद्वतापूर्ण रीति से सरल, सुबोध उदाहरणादि से सुसज्जित सपरिशिष्ट कर एक हृदय-अनवद्य टीका के साथ इस ग्रन्थ को जनता जनार्दन के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस टीका को देखकर मेरे मन में यह दृढ़ धारणा प्रादुर्भूत हुई कि अब उक्त ग्रन्थ इस विशिष्ट टीका का सम्पर्क पाकर समस्त विद्वत्माज तथा जनसाधारण के लिए अत्यन्त समादरणीय और संग्राह्य होगा। टीका की लेखन शैली से लेखक की प्रसंशनीय प्रतिभा और लोकोपकार की भावना स्फुट रुप से प्रकट होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि ज्योतिषशास्त्र में रुचि रखनेवाले सभी बन्धु इस टीका से लाभ उठाकर लेखक को अन्य कठोर ग्रन्थों को भी अपनी ललित लेखनी से कोमल बनाने के लिए उत्साहित करेंगे।
इसी आदेश के एक अंग का नाम प्रश्नावगम तन्त्र है। इस प्रश्न-प्रणाली को जैन सिद्धान्त के प्रवर्तकों ने भी आवश्यक समझकर बड़ी तत्परता से अपनाया था और उसकी सारी विचारधाराएँ ‘केवलज्ञानप्रश्नचूडामणि’ के रूप में लेखबद्ध कर सुरक्षित रखी थीं, किन्तु वह ग्रन्थ अत्यन्त दुरुह होने के कारण सर्वसाधारण का उपकार करने में पूर्णरूपेण स्वयं समर्थ नहीं रहा। अतः मेरे योग्यतम शिष्य श्री नेमिचन्द्र जैन ने बहुत ही विद्वतापूर्ण रीति से सरल, सुबोध उदाहरणादि से सुसज्जित सपरिशिष्ट कर एक हृदय-अनवद्य टीका के साथ इस ग्रन्थ को जनता जनार्दन के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस टीका को देखकर मेरे मन में यह दृढ़ धारणा प्रादुर्भूत हुई कि अब उक्त ग्रन्थ इस विशिष्ट टीका का सम्पर्क पाकर समस्त विद्वत्माज तथा जनसाधारण के लिए अत्यन्त समादरणीय और संग्राह्य होगा। टीका की लेखन शैली से लेखक की प्रसंशनीय प्रतिभा और लोकोपकार की भावना स्फुट रुप से प्रकट होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि ज्योतिषशास्त्र में रुचि रखनेवाले सभी बन्धु इस टीका से लाभ उठाकर लेखक को अन्य कठोर ग्रन्थों को भी अपनी ललित लेखनी से कोमल बनाने के लिए उत्साहित करेंगे।
-श्री रामव्यास ज्योतिषी
जैन ज्योतिष की महत्ता
भारतीय विज्ञान की उन्नति में इतर धर्मावलम्बियों के साथ कन्धे से कन्धा लगाकर चलनेवाले जैनाचार्यों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसकी अमर लेखनी से प्रसूत दिव्य रचनाएँ आज भी जैन-विज्ञान की यशःपताका को फहरा रही हैं। ज्योतिषशास्त्र के इतिहास का आलोडन करने पर ज्ञात होता है कि जैनाचार्यों द्वारा निर्मित ज्योतिष ग्रन्थों से भारतीय ज्योतिष में अनेक नवीन बातों का समावेश तथा प्रचीन सिद्धान्तों में परिमार्जित हुए हैं। जैन ग्रन्थों की सहायता के बिना भारतीय ज्योतिष के विकास-क्रम को समझना कठिन ही नहीं, असम्भव है।
भारतीय ज्योतिष का श्रृंखलाबद्ध इतिहास हमें आर्यभट्ट के समय से मिलता है। इसके पूर्ववर्ती ग्रन्थ वेद, अंगसाहित्य, ब्राह्मण, सूर्यप्रज्ञप्ति, गर्गसंहिता, ज्योतिष्करण्डक एवं वेदांगज्योतिष प्रभृति ग्रन्थों में ज्योतिषशास्त्र की अनेक महत्त्वपूर्ण बातों का वर्णन आया है। वेदांगज्योतिष में पञ्चवर्षीय युग पर से उत्तरायण और दक्षिणायन के तिथि, नक्षत्र दिनमान आदि का साधन किया है। इसके अनुसार युग का आरम्भ माघ शुक्ल प्रतिपदा के दिन सूर्य और चन्द्रमा के घनिष्ठा नक्षत्र सहित क्रान्तिवृत्त में पहुँचने पर होता है। इस ग्रन्थ का रचनाकाल कई शती ई.पू. माना जाता है। विद्वानों ने इस रचनाकाल का पता लगाने के लिए जैन ज्योतिष को ही पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार किया है। वेदांगज्योतिष पर उसके पूर्ववर्ती और समकालीन ज्योतिषकण्डक, सूर्यप्रज्ञप्ति एवं षट्खण्डागम में फुटकर उपलब्ध ज्योतिष चर्चा का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। ‘हिन्दुत्व’ को लेखक ने जैन ज्योतिष का महत्त्व और प्राचीनता स्वीकार करते हुए पृष्ठ 581 पर लिखा है—‘‘भारतीय ज्योतिष में यूनानियों की शैली का प्रचार विक्रमीय संवत से तीन सौ वर्ष पीछे हुआ। पर जैनों के मूल ग्रन्थ अंगों में यवन ज्योतिष का कुछ भी आभास नहीं है। जिस प्रकार सनातनियों की वेदसंहिता में पञ्चवर्षात्मक युग है और कृत्तिका से नक्षत्र गणना; उसी प्रकार जैन के अंग ग्रंथों में भी।’’
डॉ. श्यामशास्त्री में ‘वेदांग-ज्योतिष’ की भूमिका में बताया है—‘‘वेदांगज्योतिष के विकास में जैन ज्योतिष का बड़ा भारी सहयोग है, बिना जैन ज्योतिष के अध्ययन के वेदांगज्योतिष का अध्ययन अधूरा कहा जाएगा। भारतीय प्राचीन ज्योतिष में जैनाचार्यों के सिद्धान्त अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण हैं।’’ पंचवर्षात्मक युग का सर्वप्रथम उल्लेख जैन ग्रन्थों में ही आता है। काललोकप्रकाश, ज्योतिषकरण्डक और सूर्य्रज्ञप्ति में जिस पंचवर्षात्मक युग का निरूपण किया है, वह वेदांगज्योतिष के युग से भिन्न और प्राचीन है। ‘सूर्यप्रज्ञप्ति’ में युग का निरूपण करते हुए लिखा है-
भारतीय ज्योतिष का श्रृंखलाबद्ध इतिहास हमें आर्यभट्ट के समय से मिलता है। इसके पूर्ववर्ती ग्रन्थ वेद, अंगसाहित्य, ब्राह्मण, सूर्यप्रज्ञप्ति, गर्गसंहिता, ज्योतिष्करण्डक एवं वेदांगज्योतिष प्रभृति ग्रन्थों में ज्योतिषशास्त्र की अनेक महत्त्वपूर्ण बातों का वर्णन आया है। वेदांगज्योतिष में पञ्चवर्षीय युग पर से उत्तरायण और दक्षिणायन के तिथि, नक्षत्र दिनमान आदि का साधन किया है। इसके अनुसार युग का आरम्भ माघ शुक्ल प्रतिपदा के दिन सूर्य और चन्द्रमा के घनिष्ठा नक्षत्र सहित क्रान्तिवृत्त में पहुँचने पर होता है। इस ग्रन्थ का रचनाकाल कई शती ई.पू. माना जाता है। विद्वानों ने इस रचनाकाल का पता लगाने के लिए जैन ज्योतिष को ही पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार किया है। वेदांगज्योतिष पर उसके पूर्ववर्ती और समकालीन ज्योतिषकण्डक, सूर्यप्रज्ञप्ति एवं षट्खण्डागम में फुटकर उपलब्ध ज्योतिष चर्चा का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। ‘हिन्दुत्व’ को लेखक ने जैन ज्योतिष का महत्त्व और प्राचीनता स्वीकार करते हुए पृष्ठ 581 पर लिखा है—‘‘भारतीय ज्योतिष में यूनानियों की शैली का प्रचार विक्रमीय संवत से तीन सौ वर्ष पीछे हुआ। पर जैनों के मूल ग्रन्थ अंगों में यवन ज्योतिष का कुछ भी आभास नहीं है। जिस प्रकार सनातनियों की वेदसंहिता में पञ्चवर्षात्मक युग है और कृत्तिका से नक्षत्र गणना; उसी प्रकार जैन के अंग ग्रंथों में भी।’’
डॉ. श्यामशास्त्री में ‘वेदांग-ज्योतिष’ की भूमिका में बताया है—‘‘वेदांगज्योतिष के विकास में जैन ज्योतिष का बड़ा भारी सहयोग है, बिना जैन ज्योतिष के अध्ययन के वेदांगज्योतिष का अध्ययन अधूरा कहा जाएगा। भारतीय प्राचीन ज्योतिष में जैनाचार्यों के सिद्धान्त अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण हैं।’’ पंचवर्षात्मक युग का सर्वप्रथम उल्लेख जैन ग्रन्थों में ही आता है। काललोकप्रकाश, ज्योतिषकरण्डक और सूर्य्रज्ञप्ति में जिस पंचवर्षात्मक युग का निरूपण किया है, वह वेदांगज्योतिष के युग से भिन्न और प्राचीन है। ‘सूर्यप्रज्ञप्ति’ में युग का निरूपण करते हुए लिखा है-
सावणबहुलपडिवए बालवकरणे अभीइनक्खत्ते।
सव्वत्थ पडमसमये जुअस्स आइं वियाणाहि।।
सव्वत्थ पडमसमये जुअस्स आइं वियाणाहि।।
अर्थात् श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन अभिजित् नक्षत्र में पंचवर्षीय युग का आरम्भ होता है।
जैन ज्योतिष की प्राचीनता के अनेक सबल प्रमाण मौजूद हैं। प्राचीन जैनागम में ज्योतिषी के लिए ‘जोइसंगविउ’ शब्द का प्रयोग आया है। ‘प्रश्नव्याकरणांग’ में बताया है- ‘‘तिरियवासी पंचविहा जोइसीया देवा, वहस्सती, चंद, सूर, सुक्क, सणिच्छरा, राहू, धूमकेउ, बुद्धा य, अंगारगा य, तत्ततवणिज्ज कणगवण्णा जेयगहा जोइसियम्मि चारं चरंति, केतु य गतिरतीया। अट्ठावीसतिविहाय णक्खतरेवगणा णाणासंट्ठाणसंठियाओ य तारगाओ ठियलेस्साचारिणो य।’’ इससे स्पष्ट है कि नवग्रहों का प्रयोग ग्रहों के रूप में ई.पू. तीसरी शती से भी पहले जैनों में प्रचलित था। ‘ज्योतिष्करण्डक’ का रचनाकाल ई.पू. तीसरी या चौथी शती निश्चित है। उसमे लगन का जो निरूपण किया है, उससे भारतीय ज्योतिष की कई नवीन बातों पर प्रकाश पड़ता है।
जैन ज्योतिष की प्राचीनता के अनेक सबल प्रमाण मौजूद हैं। प्राचीन जैनागम में ज्योतिषी के लिए ‘जोइसंगविउ’ शब्द का प्रयोग आया है। ‘प्रश्नव्याकरणांग’ में बताया है- ‘‘तिरियवासी पंचविहा जोइसीया देवा, वहस्सती, चंद, सूर, सुक्क, सणिच्छरा, राहू, धूमकेउ, बुद्धा य, अंगारगा य, तत्ततवणिज्ज कणगवण्णा जेयगहा जोइसियम्मि चारं चरंति, केतु य गतिरतीया। अट्ठावीसतिविहाय णक्खतरेवगणा णाणासंट्ठाणसंठियाओ य तारगाओ ठियलेस्साचारिणो य।’’ इससे स्पष्ट है कि नवग्रहों का प्रयोग ग्रहों के रूप में ई.पू. तीसरी शती से भी पहले जैनों में प्रचलित था। ‘ज्योतिष्करण्डक’ का रचनाकाल ई.पू. तीसरी या चौथी शती निश्चित है। उसमे लगन का जो निरूपण किया है, उससे भारतीय ज्योतिष की कई नवीन बातों पर प्रकाश पड़ता है।
लग्गं च दक्खिणायविसुदेसुवि अस्स उत्तरं अयणे।
लग्गं साई विसुवेसु पंचषु वि दक्खिणे अयणे।।
लग्गं साई विसुवेसु पंचषु वि दक्खिणे अयणे।।
इस पद्य में ‘अस्स’ यानी अश्विनी और ‘साई’ यानी स्वाती ये विषुव के लग्न बताये गये हैं। ‘ज्योतिष्कण्डक’ में विशिष्ट अवस्था के नक्षत्रों को भी लग्न कहा गया है। यवनों के आगमन के पूर्व भारत में यही जैन लग्नप्रणाली प्रचलित थी। ‘वेदांगज्योतिष’ में भी इस लग्नप्रणाली का आभास मिलता है- ‘‘श्रविष्ठाभ्यां गुणाभ्यस्तान् प्राविलग्नान् विनिर्दिशेत्’’ इस पद्यार्थ में वर्तमान लग्न नक्षत्रों का निरूपण किया गया है। प्राचीन भारत में विशिष्ट अवस्था की राशि के समान विशिष्ट अवस्था के नक्षत्रों को भी लग्न कहा जाता था।...
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book