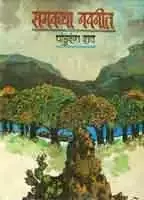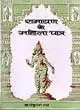|
धर्म एवं दर्शन >> रामकथा नवनीत रामकथा नवनीतपांडुरंग राव
|
121 पाठक हैं |
||||||
रामायण केवल राम की कहानी नहीं है, वह राम का अयन है- केवल राम का नहीं, बल्कि रामा (सीता) का भी।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
रामायण केवल राम की कहानी नहीं है, वह राम का अयन है- केवल राम का नहीं,
बल्कि रामा (सीता) का भी। दोनों का समन्वित अयन ही रामायण है। राम और रामा में रमणीयता है तो अयन में गतिशीलता है। इसीलिए रामायण की रमणीयता गतिशील है। वह तमसा नदी के स्वच्छ जल की तरह प्रसन्न और रमणीय भी है और क्रौंच-मिथुन के क्रंदन की तरह करुणाकलित भी है। राम प्रेम के प्रतीक हैं तो सीता करुणा की मूर्ति हैं। मानव-जीवन के इन दोनों मूल्यों को आधार बनाकर वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है जिसमें पृथ्वी और आकाश, गंध और माधुर्य तथा सत्य और सौन्दर्य का मंजुल सामंजस्य कथा को अयन का गौरव प्रदान करता है। जीवन की पुकार रामायण की जीवन-नाड़ी है। जीना और जीने देना रामायणीय संस्कृति का मूल मंत्र है और इसी में रामकथा भारती की
लोकप्रियता का रहस्य है।
भारतीय जनजीवन में ही नहीं, बल्कि विश्व-संस्कृति में भी वाल्मीकि की इस अमर कृति का विशिष्ट स्थान है। जीवन के हर प्रसंग में रामायण की याद आती है और हर व्यक्ति की जीवनी राम कहानी-सी लगती है। समता, ममता और समरसता पर आधारित मानव जीवन की इसी मधुर मनोहारिता का मार्मिक चित्रण ही आर्ष कवि की अनर्घ सृष्टि का बीज है। यही बीज रामायण के विविध प्रसंगों में क्रमशः पल्लवित होकर अंत में राम-राज्य के शुभोदय में सुन्दर पारिजात के रूप में विकसित होता है। यही रामायण का परमार्थ है, रामकथा नवनीत है और यही है आदिकवि का आत्मदर्शन।
प्रस्तुत है इस महनीय कृति का नवीन संस्करण।
भारतीय जनजीवन में ही नहीं, बल्कि विश्व-संस्कृति में भी वाल्मीकि की इस अमर कृति का विशिष्ट स्थान है। जीवन के हर प्रसंग में रामायण की याद आती है और हर व्यक्ति की जीवनी राम कहानी-सी लगती है। समता, ममता और समरसता पर आधारित मानव जीवन की इसी मधुर मनोहारिता का मार्मिक चित्रण ही आर्ष कवि की अनर्घ सृष्टि का बीज है। यही बीज रामायण के विविध प्रसंगों में क्रमशः पल्लवित होकर अंत में राम-राज्य के शुभोदय में सुन्दर पारिजात के रूप में विकसित होता है। यही रामायण का परमार्थ है, रामकथा नवनीत है और यही है आदिकवि का आत्मदर्शन।
प्रस्तुत है इस महनीय कृति का नवीन संस्करण।
प्रस्तुति
प्रथम संस्करण से
भारतीय साहित्य में रामायण एक ऐसी रचना है जो भारत की प्रत्येक भाषा में
किसी न किसी रूप में उपलब्ध है। भारत की सांस्कृतिक चेतना, साहित्यिक
प्रेरणा, और सामाजिक भावना को मूल आधार प्रदान करनेवाला यह अमर काव्य
आदिकवि वाल्मीकि की देन है। देश-विदेश में राम काव्य के अनेक रूप देखने को
मिलते हैं, पर मूल वस्तु वाल्मीकि की मौलिक उद्भावना है। आदिकवि से
प्रेरणा पाकर ही सैकड़ों कवियों ने अपनी-अपनी रुचि और अपने समय की सामाजिक
स्थिति के अनुसार रामकथा के विभिन्न रूपांतर प्रस्तुत किये हैं। राम काव्य
की इस विराट् परम्परा को हृदयंगम करने के लिए वाल्मीकि की रामायण को समग्र
रूप से समझना आवश्यक है। प्रस्तुत रचना रामकथा नवनीत इसी आवश्यकता की
पूर्ति करती है।
इस ग्रंथ के प्रणेता, शब्दों के अनन्य पारखी तथा रामायण-साहित्य के अधिकारी विद्वान् डॉ. पांडुरंग राव के शब्दों में, रामायण वास्तव में भारत का ज्ञानपीठ है। इसीलिए भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा रामकथा नवनीत का प्रकाशित होना सर्वथा उचित और समीचीन है। इसे मैं ज्ञानपीठ के लिए सौभाग्य की बात समझता हूँ। आशा है, सुधी पाठक इस प्रकाशन का स्वागत करेंगे।
इस ग्रंथ के प्रणेता, शब्दों के अनन्य पारखी तथा रामायण-साहित्य के अधिकारी विद्वान् डॉ. पांडुरंग राव के शब्दों में, रामायण वास्तव में भारत का ज्ञानपीठ है। इसीलिए भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा रामकथा नवनीत का प्रकाशित होना सर्वथा उचित और समीचीन है। इसे मैं ज्ञानपीठ के लिए सौभाग्य की बात समझता हूँ। आशा है, सुधी पाठक इस प्रकाशन का स्वागत करेंगे।
रमेश चन्द्र न्यासी
अथ
प्रथम संस्करण से
भारतीय जन-जीवन को सच्चे अर्थों में भारतीयता (प्रकाश के प्रति प्रेम) से
अनुप्राणित करनेवाले दो आलोक-पुंज हैं-प्रभाकर और सुधाकर। प्रभाकर अथवा
सूर्य दिन को गतिशील बनाता है और सुधाकर अथवा चंद्रमा रात को सुहावनी
बनाता है। दोनों एक-दूसरे के प्रेरक और पूरक हैं। सूर्यवंश में सूर्य का
तेज लेकर मध्याह्न के समय अवतरित दशरथ नंदन राम और यदुकुल में चंद्रमा के
साथ-साथ आधी रात के समय प्रादुर्भूत देवकी नंदन कृष्ण वास्तव में सूर्य और
चंद्र के ही प्रतिरूप हैं। इसीलिए जब तक सूर्य और चंद्र दिन-रात को आलोकित
और आवासित करते रहते हैं, तब तक राम और कृष्ण की रमणीय और कमनीय
कथा-माधुरी लोक को आलोक प्रदान करती रहेगी। दोनों अपने युग के निर्माता और
युग-धर्म के संस्थापक रहे। धर्म का संस्थापन दोनों का ध्येय था, पर राम ने
सत्य के आधार पर धर्म का पालन किया तो कृष्ण ने न्याय का अवलंब लेकर धर्म
को प्रतिष्ठित किया। सत्य और धर्म के मूर्तरूप थे तो कृष्ण धर्म के प्रतीक
थे। राम प्रेम प्रतिरूप थे तो कृष्ण प्रेम के उपासक थे। राम का लक्ष्य
‘शुभ’ था और कृष्ण का ध्येय ‘जय’
था। राम दिन के
मार्तंड थे तो कृष्ण रात के राकेश थे। पर थे दोनों प्रकाश के पुंज।
इन्हीं दो आलोक-पुंजों की आभा से प्रतिभासित कालजयी कृतियाँ हैं-रामायण और महाभारत। रामायण में ज्ञान का प्रकाश धर्म को सत्य का आलोक प्रदान करता है तो महाभारत में प्रतिपादित कर्तव्य कर्म का आचरण न्याय को धर्मसम्मत बनाता है। रामायण ज्ञान-पीठ है तो महाभारत कर्म-भूमि है। रामायण से ज्ञान का आलोक और महाभारत से कर्म का लोक लेकर ही श्रीमद्भागवत ने इच्छा-जगत् और स्वच्छंद रसवाहिनी से युक्त भक्ति मंदाकिनी को प्रवाहित किया है। रामायण का ज्ञान, महाभारत का कर्म और श्रीमद्भागत् की इच्छा इन्हीं तीन सूत्रों से आबद्ध होकर आर्ष वाणी भारतभारती को भारतीय बनाती है। इसलिए भारतीय साहित्य, दर्शन और संस्कृति के आधार-त्रयी कहलाने योग्य ये तीनों ग्रंथ भारतीयता को पहचानने में अत्यंत सहायक ही नहीं, बल्कि अपरिहार्य साधन सिद्ध होते हैं।
इनमें रामायण का एक विशिष्ट स्थान है क्योंकि वह ज्ञान का भंडार है। कर्म और धर्म के बीच समन्वय स्थापित करनेवाले महाभारत की मध्यधरा श्रीमद्भगवतगीता का निश्चित मत है कि ज्ञान से बढ़कर पवित्र वस्तु इस संसार में और कुछ नहीं है और आचार्य शंकर भी मुक्त कंठ से ज्ञान को मुक्ति का एकमात्र साधन घोषित करते हैं। सत्य और धर्म, भक्ति और मुक्ति भोग, और त्याग, अनुराग और विराग इन सबका समन्वय प्रस्तुत करनेवाली प्रशस्त रचना रामायण वास्तव में भारतीयता का अक्षय कोश है। महाभारत के संबंध में प्रायः कहा जाता है कि जो महाभारत में नहीं है, वह भारत में भी नहीं है। यही बात रामायण के संबंध में भी चरितार्थ होती है, बल्कि रामायण के संबंध में एक कदम आगे बढ़कर यह कहा जा सकता है कि जो रामायण में नहीं है वह विश्व में भी नहीं है, क्योंकि रामायण केवल भारत की ही संपत्ति नहीं है, बल्कि वह मानव मात्र की महिमा का गुणगान करनेवाली विश्वजनीय रचना है। वह देश, काल और व्यक्ति की परिकल्पित सीमाओं से परे है।
रामायण की मूल शक्ति ज्ञान है जिसके कई पहलू हैं। कभी वह शब्द के रूप में व्यक्त होता है, कभी विचार के रूप में, कभी संचरण के रूप में हमारे साथ चलता है और कभी आचरण के रूप में हमें चलना सिखाता है। कभी-कभी वह मौन धारण कर हमारे मन को मुखरित कर देता है और कभी मनन बनकर मन में नमन की भावना पैदा कर देता है। कभी आज्ञा बनकर हमें आदेश देता है और कभी संज्ञा बनकर संदेश का सारा सुनाता है। कभी प्रज्ञा बनकर पंडितों को प्रबुद्ध बनाता और कभी विद्या बनकर विज्ञ को विद्वान बना देता। कभी कर्म की भावना जगाता है और कभी धर्म का रहस्य खोलता है। कभी मुक्ति का मार्ग दिखाता है और कभी भक्ति का गीत सुनाता है। संक्षेप में रामायण जिस अर्थ में ज्ञान का पीठ माना जा सकता है उस अर्थ में यह ज्ञान संसार का सर्वस्व है और समस्त साधना का सार है।
रामायण केवल कहानी नहीं है, वह अयन भी है। कहानी और अयन में काफी अंतर है। इसीलिए आदिकवि वाल्मीकि ने अपनी कृति का नाम ‘रामायण’ रखा। यदि यह कथा है तो रामायण-कथा है, केवल राम कथा नहीं। ‘‘तावद् रामायण-कथा लोकेषु प्रचरिष्यति’’-आदि सूक्तियों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। यह चरित भी नहीं है क्योंकि चलना समय सापेक्ष और क्षणिक होता है जब कि रामायण का चरित शाश्वत है (इदं हि चरितं लोके विस्तृति को लोक शब्द से युक्त किया गया है। लोक भी एक नहीं, अनेक हैं। जहाँ तक आलोक है वहाँ तक रामायण का लोक व्याप्त है। इसलिए रामायण को कथा, चरित आदि कहना उसके लोक की अवधि या परिधि को परिमित करना होगा। तभी तो वाक्य कोविद वाल्मीकि ने इस कृति को रामायण की संज्ञा दी है। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास ने भी ‘‘यद् रामायणे निगदितम्’’ कहकर ‘रामायण’ शब्द मात्र से वाल्मीकि रामायण की ओर विवेकपूर्ण संकेत किया है। केवल ‘रामायण’ कहना पर्याप्त है, वाल्मीकि का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ‘रामायण’ शब्द वाल्मीकि की अपनी निजी और परिनिष्ठित उद्भावना है।
अयन में केवल कहानी नहीं होती है, केवल घटना नहीं होती है, केवल चरित्र-चित्रण नहीं होता है, केवल चमत्कार, रस, अलंकार, ध्वनि, गुण आदि नहीं होते हैं-ये सब हो सकते हैं, पर इनके अतिरिक्त और भी बहुत-सी बातें होती हैं जो ‘अयन’ की विस्तृत परिधि में आती हैं। वास्तव में अयन गतिशीलता का द्योतक है और यह अयन राम का होने के कारण रमणीयता का भी सूचक है। ‘रामायण’ में इन्हीं दो का रासायनिक संयोग है। वह नदी के प्रवाह की भाँति गतिशील भी है और निर्मल जल के उर्मिल उत्थान की भाँति रमणीय भी है। ‘राम’ शब्द में जो रमणीयता है और ‘अयन’ शब्द में जो गतिशीलता है-दोनों का मणि-कांचन संयोग ही रामायण है। राम अपने जीवन में क्या करते थे, क्या पाते और क्या खाते थे, यह सब उनके अयन का कथन मात्र बन सकता है, पर कथ्य नहीं और कथ्य बिल्कुल नहीं। ‘अयन’ के अंतर्गत राम की मुद्रा, दृष्टि, मनस्विता, तपस्या, वाग्मिता, तेजस्विता, ओजस्विता, वर्चस्विता आदि में सम्मिलित समस्त अंतरंग-विभूति आती है जिससे इस अमोघ रचना के अध्येताओं को राम के अयन की अनुभूति होती है। इस दृष्टि से रामायण अनर्घराघव की आंतरिक अनुभूति है जिसे आदिकवि ने अभिव्यक्त का रूप दिया है।
राम क्या करते थे, यह रामायण का कथ्य नहीं है। पर कैसे करते थे, कैसे बैठते थे, कैसे देखते थे, कैसे सोचते थे और कैसे प्रापंचिक अनुभूति को आत्मसात् करते थे, यही रामायण का मननीय अंश है और इसी मनन में राम के अयन का वास्तविक महत्त्व है। एक और विशेषता इस अयन की यह है कि इसमें केवल राम का एकांगी अयन नहीं है, बल्कि यह सीता और राम का समन्वित और समेकित अयन है। रामायण शब्द में ही यह समन्वय भावना है। असल में यह राम और रामा-दोनों का अयन है। इसी में रामायण के नामकरण की सार्थकता और सारवत्ता है। राम का अयन और रामा का अयन-दोनों प्रकार से रामायण शब्द का विग्रह किया जा सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि शब्द ब्रह्म के वेत्ता वाल्मीकि ने यहाँ पर सीता के लिए रामा शब्द का प्रयोग किया है और कथा, चरित गाथा आदि के स्थान पर अयन शब्द को अधिक उपयुक्त समझा। तभी तो रामायण जैसा रमणीय नामकरण रामायण की ध्वन्यात्मक प्रवृत्ति का स्फुरण कराने में समर्थ हो पाया है। सीता के लिए ‘रामा’ शब्द का प्रयोग केवल चमत्कारिक नहीं है, बल्कि वाल्मीकि के लिए यह प्रयोग अत्यंत स्वाभाविक सरल और अभीष्ट है। रामायण में अनेक प्रसंगों पर यह प्रयोग मिलता है। ‘रामायण’ को राम और रामा का समन्वित और पुरुष की पारस्परिक परिपूरकता की ओर भी सात्त्विक संकेत मिलता है। इस प्रकार वाल्मीकि ने पुरुषोत्तम राम की इस परम रमणीय कथा को ‘अयन’ का रूप दिया, तो यह रामकथा नवनीत उसी अयन का अध्ययन प्रस्तुत करता है-एक ‘अल्पविषयामति’ अध्येता की अनधिकार चेष्टा के रूप में।
रामायण के संबंध में कुछ कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। यह बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि इस सरल से सरल किंतु दुरूह रचना को जब कभी मैं समझने की चेष्टा करता हूँ तो बात यही समझ में आती है कि जब तक मैं अपने को समझ नहीं पाऊँ तब तक आदिकवि का यह आत्मदर्शन आंशिक रूप से ही सही, समझ में नहीं आ सकता। इसलिए रामायण, मेरी दृष्टि में, आदिकवि के आत्मदर्शन का ही प्रामाणिक प्रणयन है। वास्तव में यह इस पंचभूत जगत् के प्रत्येक प्राणी का प्राणायन है। अमूर्त प्राण को मूर्त रूप देकर वाल्मीकि ने सीता राम की सुंदर मूर्ति को संसार के सामने प्रतिष्ठित किया है जिसे प्राणी अपने अपने संस्कार अनुरूप अपने अंतरंग में आत्मसात् कर सकता है। इसी प्रयास का परिणाम है-यह नवनीत। इसमें कितना नीत है, कितना अनीत या विनीत, यह नय और विनय के मर्मज्ञ और सहृदय पाठक ही निर्णय कर सकते हैं। पर मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि जैसे मेरे, वैसे सबके अंतरंग में प्रतिष्ठित आत्माराम ने जितनी आत्मरति मुझे प्रसाद के रूप में प्रदान की है, उतनी ही में मेरा आत्मतोष है।
आदिकवि के लिए जो आत्मदर्शन था, वही गुणग्राही पाठक समाज के लिए जीवन दर्शन बन गया है। यही रामायण का सच्चा और सार्थक दर्शन है। जीवन का प्रमुख आधार जिजीविषा (जीने की इच्छा) है जो कि रामायण की भाव-भूमिका का भी मूल है। नारद के श्रीमुख से आदर्श राम का गुणगान सुनने के बाद जब तपस्वी वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर टहलने जाते हैं तो उनके सामने दो दृश्य दिखाई देते हैं-तमसा का तरल सरल प्रवाह और निषाद के निष्ठुर प्रहार का शिकार क्रौंच पक्षी। तमसा का निर्मल जल देखकर तपस्वी का मन जितना प्रसन्न होता है, क्रौंच-मिथुन के आकस्मिक वियोग को देखकर उतना ही आक्रांत हो जाता है। तमसा नदी का प्रवाह जीवन की सरलता, स्वच्छता और गतिशीलता को प्रेरणा प्रदान करता है तो क्रौंच-मिथुन के ऐकांतिक सुख में अचानक उत्पन्न आघात जीने और जीने देने की सहज मानवीय लालसा को रक्त-सिक्त और विच्छिन्न बना देता है। मनस्वी महर्षि सोचने लगते हैं कि आखिर मानव इतना निष्ठुर क्यों होता है और वह भी अकारण ? जल की तरंगों के समान निर्मल और उर्मिल जीवन-प्रवाह का अभिन्न अंग बनकर चलनेवाला प्राणी अचानक इतना आत्मघाती क्यों बन जाता है ? अपने साथ जीवन का आनंद लेनेवाले सहजीवियों को जीने के अधिकार से वंचित करनेवाले जीवी को जीने का क्या अधिकार है ? इसी प्रकार के प्रश्न प्राचेतस के मन को झकझोरते हैं, उनके अंतर्मन में अशांति का चक्रवात उत्पन्न करते हैं और उनके भीतर का शोक बाहर श्लोक बनकर प्रकट होता है :
इन्हीं दो आलोक-पुंजों की आभा से प्रतिभासित कालजयी कृतियाँ हैं-रामायण और महाभारत। रामायण में ज्ञान का प्रकाश धर्म को सत्य का आलोक प्रदान करता है तो महाभारत में प्रतिपादित कर्तव्य कर्म का आचरण न्याय को धर्मसम्मत बनाता है। रामायण ज्ञान-पीठ है तो महाभारत कर्म-भूमि है। रामायण से ज्ञान का आलोक और महाभारत से कर्म का लोक लेकर ही श्रीमद्भागवत ने इच्छा-जगत् और स्वच्छंद रसवाहिनी से युक्त भक्ति मंदाकिनी को प्रवाहित किया है। रामायण का ज्ञान, महाभारत का कर्म और श्रीमद्भागत् की इच्छा इन्हीं तीन सूत्रों से आबद्ध होकर आर्ष वाणी भारतभारती को भारतीय बनाती है। इसलिए भारतीय साहित्य, दर्शन और संस्कृति के आधार-त्रयी कहलाने योग्य ये तीनों ग्रंथ भारतीयता को पहचानने में अत्यंत सहायक ही नहीं, बल्कि अपरिहार्य साधन सिद्ध होते हैं।
इनमें रामायण का एक विशिष्ट स्थान है क्योंकि वह ज्ञान का भंडार है। कर्म और धर्म के बीच समन्वय स्थापित करनेवाले महाभारत की मध्यधरा श्रीमद्भगवतगीता का निश्चित मत है कि ज्ञान से बढ़कर पवित्र वस्तु इस संसार में और कुछ नहीं है और आचार्य शंकर भी मुक्त कंठ से ज्ञान को मुक्ति का एकमात्र साधन घोषित करते हैं। सत्य और धर्म, भक्ति और मुक्ति भोग, और त्याग, अनुराग और विराग इन सबका समन्वय प्रस्तुत करनेवाली प्रशस्त रचना रामायण वास्तव में भारतीयता का अक्षय कोश है। महाभारत के संबंध में प्रायः कहा जाता है कि जो महाभारत में नहीं है, वह भारत में भी नहीं है। यही बात रामायण के संबंध में भी चरितार्थ होती है, बल्कि रामायण के संबंध में एक कदम आगे बढ़कर यह कहा जा सकता है कि जो रामायण में नहीं है वह विश्व में भी नहीं है, क्योंकि रामायण केवल भारत की ही संपत्ति नहीं है, बल्कि वह मानव मात्र की महिमा का गुणगान करनेवाली विश्वजनीय रचना है। वह देश, काल और व्यक्ति की परिकल्पित सीमाओं से परे है।
रामायण की मूल शक्ति ज्ञान है जिसके कई पहलू हैं। कभी वह शब्द के रूप में व्यक्त होता है, कभी विचार के रूप में, कभी संचरण के रूप में हमारे साथ चलता है और कभी आचरण के रूप में हमें चलना सिखाता है। कभी-कभी वह मौन धारण कर हमारे मन को मुखरित कर देता है और कभी मनन बनकर मन में नमन की भावना पैदा कर देता है। कभी आज्ञा बनकर हमें आदेश देता है और कभी संज्ञा बनकर संदेश का सारा सुनाता है। कभी प्रज्ञा बनकर पंडितों को प्रबुद्ध बनाता और कभी विद्या बनकर विज्ञ को विद्वान बना देता। कभी कर्म की भावना जगाता है और कभी धर्म का रहस्य खोलता है। कभी मुक्ति का मार्ग दिखाता है और कभी भक्ति का गीत सुनाता है। संक्षेप में रामायण जिस अर्थ में ज्ञान का पीठ माना जा सकता है उस अर्थ में यह ज्ञान संसार का सर्वस्व है और समस्त साधना का सार है।
रामायण केवल कहानी नहीं है, वह अयन भी है। कहानी और अयन में काफी अंतर है। इसीलिए आदिकवि वाल्मीकि ने अपनी कृति का नाम ‘रामायण’ रखा। यदि यह कथा है तो रामायण-कथा है, केवल राम कथा नहीं। ‘‘तावद् रामायण-कथा लोकेषु प्रचरिष्यति’’-आदि सूक्तियों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। यह चरित भी नहीं है क्योंकि चलना समय सापेक्ष और क्षणिक होता है जब कि रामायण का चरित शाश्वत है (इदं हि चरितं लोके विस्तृति को लोक शब्द से युक्त किया गया है। लोक भी एक नहीं, अनेक हैं। जहाँ तक आलोक है वहाँ तक रामायण का लोक व्याप्त है। इसलिए रामायण को कथा, चरित आदि कहना उसके लोक की अवधि या परिधि को परिमित करना होगा। तभी तो वाक्य कोविद वाल्मीकि ने इस कृति को रामायण की संज्ञा दी है। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास ने भी ‘‘यद् रामायणे निगदितम्’’ कहकर ‘रामायण’ शब्द मात्र से वाल्मीकि रामायण की ओर विवेकपूर्ण संकेत किया है। केवल ‘रामायण’ कहना पर्याप्त है, वाल्मीकि का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ‘रामायण’ शब्द वाल्मीकि की अपनी निजी और परिनिष्ठित उद्भावना है।
अयन में केवल कहानी नहीं होती है, केवल घटना नहीं होती है, केवल चरित्र-चित्रण नहीं होता है, केवल चमत्कार, रस, अलंकार, ध्वनि, गुण आदि नहीं होते हैं-ये सब हो सकते हैं, पर इनके अतिरिक्त और भी बहुत-सी बातें होती हैं जो ‘अयन’ की विस्तृत परिधि में आती हैं। वास्तव में अयन गतिशीलता का द्योतक है और यह अयन राम का होने के कारण रमणीयता का भी सूचक है। ‘रामायण’ में इन्हीं दो का रासायनिक संयोग है। वह नदी के प्रवाह की भाँति गतिशील भी है और निर्मल जल के उर्मिल उत्थान की भाँति रमणीय भी है। ‘राम’ शब्द में जो रमणीयता है और ‘अयन’ शब्द में जो गतिशीलता है-दोनों का मणि-कांचन संयोग ही रामायण है। राम अपने जीवन में क्या करते थे, क्या पाते और क्या खाते थे, यह सब उनके अयन का कथन मात्र बन सकता है, पर कथ्य नहीं और कथ्य बिल्कुल नहीं। ‘अयन’ के अंतर्गत राम की मुद्रा, दृष्टि, मनस्विता, तपस्या, वाग्मिता, तेजस्विता, ओजस्विता, वर्चस्विता आदि में सम्मिलित समस्त अंतरंग-विभूति आती है जिससे इस अमोघ रचना के अध्येताओं को राम के अयन की अनुभूति होती है। इस दृष्टि से रामायण अनर्घराघव की आंतरिक अनुभूति है जिसे आदिकवि ने अभिव्यक्त का रूप दिया है।
राम क्या करते थे, यह रामायण का कथ्य नहीं है। पर कैसे करते थे, कैसे बैठते थे, कैसे देखते थे, कैसे सोचते थे और कैसे प्रापंचिक अनुभूति को आत्मसात् करते थे, यही रामायण का मननीय अंश है और इसी मनन में राम के अयन का वास्तविक महत्त्व है। एक और विशेषता इस अयन की यह है कि इसमें केवल राम का एकांगी अयन नहीं है, बल्कि यह सीता और राम का समन्वित और समेकित अयन है। रामायण शब्द में ही यह समन्वय भावना है। असल में यह राम और रामा-दोनों का अयन है। इसी में रामायण के नामकरण की सार्थकता और सारवत्ता है। राम का अयन और रामा का अयन-दोनों प्रकार से रामायण शब्द का विग्रह किया जा सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि शब्द ब्रह्म के वेत्ता वाल्मीकि ने यहाँ पर सीता के लिए रामा शब्द का प्रयोग किया है और कथा, चरित गाथा आदि के स्थान पर अयन शब्द को अधिक उपयुक्त समझा। तभी तो रामायण जैसा रमणीय नामकरण रामायण की ध्वन्यात्मक प्रवृत्ति का स्फुरण कराने में समर्थ हो पाया है। सीता के लिए ‘रामा’ शब्द का प्रयोग केवल चमत्कारिक नहीं है, बल्कि वाल्मीकि के लिए यह प्रयोग अत्यंत स्वाभाविक सरल और अभीष्ट है। रामायण में अनेक प्रसंगों पर यह प्रयोग मिलता है। ‘रामायण’ को राम और रामा का समन्वित और पुरुष की पारस्परिक परिपूरकता की ओर भी सात्त्विक संकेत मिलता है। इस प्रकार वाल्मीकि ने पुरुषोत्तम राम की इस परम रमणीय कथा को ‘अयन’ का रूप दिया, तो यह रामकथा नवनीत उसी अयन का अध्ययन प्रस्तुत करता है-एक ‘अल्पविषयामति’ अध्येता की अनधिकार चेष्टा के रूप में।
रामायण के संबंध में कुछ कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। यह बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि इस सरल से सरल किंतु दुरूह रचना को जब कभी मैं समझने की चेष्टा करता हूँ तो बात यही समझ में आती है कि जब तक मैं अपने को समझ नहीं पाऊँ तब तक आदिकवि का यह आत्मदर्शन आंशिक रूप से ही सही, समझ में नहीं आ सकता। इसलिए रामायण, मेरी दृष्टि में, आदिकवि के आत्मदर्शन का ही प्रामाणिक प्रणयन है। वास्तव में यह इस पंचभूत जगत् के प्रत्येक प्राणी का प्राणायन है। अमूर्त प्राण को मूर्त रूप देकर वाल्मीकि ने सीता राम की सुंदर मूर्ति को संसार के सामने प्रतिष्ठित किया है जिसे प्राणी अपने अपने संस्कार अनुरूप अपने अंतरंग में आत्मसात् कर सकता है। इसी प्रयास का परिणाम है-यह नवनीत। इसमें कितना नीत है, कितना अनीत या विनीत, यह नय और विनय के मर्मज्ञ और सहृदय पाठक ही निर्णय कर सकते हैं। पर मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि जैसे मेरे, वैसे सबके अंतरंग में प्रतिष्ठित आत्माराम ने जितनी आत्मरति मुझे प्रसाद के रूप में प्रदान की है, उतनी ही में मेरा आत्मतोष है।
आदिकवि के लिए जो आत्मदर्शन था, वही गुणग्राही पाठक समाज के लिए जीवन दर्शन बन गया है। यही रामायण का सच्चा और सार्थक दर्शन है। जीवन का प्रमुख आधार जिजीविषा (जीने की इच्छा) है जो कि रामायण की भाव-भूमिका का भी मूल है। नारद के श्रीमुख से आदर्श राम का गुणगान सुनने के बाद जब तपस्वी वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर टहलने जाते हैं तो उनके सामने दो दृश्य दिखाई देते हैं-तमसा का तरल सरल प्रवाह और निषाद के निष्ठुर प्रहार का शिकार क्रौंच पक्षी। तमसा का निर्मल जल देखकर तपस्वी का मन जितना प्रसन्न होता है, क्रौंच-मिथुन के आकस्मिक वियोग को देखकर उतना ही आक्रांत हो जाता है। तमसा नदी का प्रवाह जीवन की सरलता, स्वच्छता और गतिशीलता को प्रेरणा प्रदान करता है तो क्रौंच-मिथुन के ऐकांतिक सुख में अचानक उत्पन्न आघात जीने और जीने देने की सहज मानवीय लालसा को रक्त-सिक्त और विच्छिन्न बना देता है। मनस्वी महर्षि सोचने लगते हैं कि आखिर मानव इतना निष्ठुर क्यों होता है और वह भी अकारण ? जल की तरंगों के समान निर्मल और उर्मिल जीवन-प्रवाह का अभिन्न अंग बनकर चलनेवाला प्राणी अचानक इतना आत्मघाती क्यों बन जाता है ? अपने साथ जीवन का आनंद लेनेवाले सहजीवियों को जीने के अधिकार से वंचित करनेवाले जीवी को जीने का क्या अधिकार है ? इसी प्रकार के प्रश्न प्राचेतस के मन को झकझोरते हैं, उनके अंतर्मन में अशांति का चक्रवात उत्पन्न करते हैं और उनके भीतर का शोक बाहर श्लोक बनकर प्रकट होता है :
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम: शाश्वतीः समा:।
यत्क्रौंचमिथुनादेकमवधी : काममोहितम्।।
यत्क्रौंचमिथुनादेकमवधी : काममोहितम्।।
भारतीय साहित्य की यह प्रथम सारस्वत अभिव्यंजना केवल आदिकवि के आदिकाव्य
का अक्षर बीज ही नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि का बीजाक्षर है। यही सृष्टि बीज
समस्त रामायण को अभीष्ट पुष्टि प्रदान कर उसे इष्ट काव्य का रूप देता है।
यज्ञ का दूसरा नाम ही इष्टि है और यज्ञ की भावना से किया गया कर्म ही धर्म
का रूप धारण करता है। प्रत्येक प्राणी प्रारंभ में अन्नजीवी बनकर अपनी
जीवन यात्रा का आरंभ करता है और धीरे-धीरे प्राण, मन और विज्ञान के
सोपानों को पारकर वह अतंतः आनंदजीवी बन जाता है। अन्न से प्राणों का
प्रणयन होता है, वर्षा से अन्न पैदा होता है और वर्षा तभी होती है जब धरती
तप-तप कर यज्ञ में अपनी रसमय आहुति देती है। यह सारी प्रक्रिया आंतरिक
प्रेरणा और अपरिहार्य कर्तव्य भावना से संपन्न होती है जिसे हम याग, योग
अथवा इष्टि का नाम दे सकते हैं।
रामकथा का उपक्रम इसी प्रकार की इष्टि से होता है जिसे वशिष्ट ऋष्यश्रृंग ऋषि मुनियों ने पुत्रकामेष्टि की संज्ञा दी। इसी इष्टि के फलस्वरूप राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। रामकथा का समापन भी अश्वमेध नाम की इष्टि से होता है। इस प्रकार रामायण के उपक्रम और उपसंहार में इष्टि की भावना विद्यमान है और इस दृष्टि से उसको इष्टिकाव्य कहा जा सकता है। विशेषकर बालकांड का सारा घटना क्रम इसी इष्टि योजना से अनुप्राणित है। दशरथ द्वारा अनुष्ठित पुत्रकोमेष्टि के फलस्वरूप राम का जन्म होता है तो सिद्धाश्रम में संपन्न होनेवाले एक विशिष्ट यज्ञ (इष्टि) की रक्षा के लिए राम को अपने साथ ले जाने विश्वामित्र एक दिन अचानक दशरथ के पास आ पहुँचते हैं। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा संपन्न होते ही मिथिला के राजा जनक द्वारा अनुष्ठित धर्नुयर्ज्ञ में सम्मिलित होने के लिए विश्वामित्र के साथ उन्हीं के अनुरोध या संकेत पर राम और लक्ष्मण मिथला पहुँचते हैं। इस प्रकार अयोध्या का यज्ञ राम को अवतरित कर देता है तो सिद्धाश्रम का यज्ञ राम को असत् के निराकरण और सत् के संस्थापन के लिए सन्नद्ध बना देता है और मिथिला का यज्ञ दशरथनंदन को सीतापति बना देता है। इस प्रकार बालकांड में तीन विशिष्ट इष्टियों की श्रृंखला दिखाई देती है जिससे अयोध्या के राजपरिवार को तो इष्ट सिद्धि होती ही है, साथ ही, समस्त राम परिवार को इष्ट लाभ भी होता है।
सीता और राम का विवाह भी अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण इष्टि है, क्योंकि सीता-राम का समागम केवल एक साधारण नर नारी का संगम नहीं है, वह धरती और आकाश का मिलन है, सुगंध और माधुर्य का सम्मिश्रण है तो सौंदर्य और सत्य का समेकन है। बालकांड में संपन्न प्रत्येक इष्टि में समष्टि की भावना स्पष्ट दिखाई देती है और यही समष्टि भावना सीता-राम के समागम का भी सत्त्व सार है।
रामकथा का उपक्रम इसी प्रकार की इष्टि से होता है जिसे वशिष्ट ऋष्यश्रृंग ऋषि मुनियों ने पुत्रकामेष्टि की संज्ञा दी। इसी इष्टि के फलस्वरूप राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। रामकथा का समापन भी अश्वमेध नाम की इष्टि से होता है। इस प्रकार रामायण के उपक्रम और उपसंहार में इष्टि की भावना विद्यमान है और इस दृष्टि से उसको इष्टिकाव्य कहा जा सकता है। विशेषकर बालकांड का सारा घटना क्रम इसी इष्टि योजना से अनुप्राणित है। दशरथ द्वारा अनुष्ठित पुत्रकोमेष्टि के फलस्वरूप राम का जन्म होता है तो सिद्धाश्रम में संपन्न होनेवाले एक विशिष्ट यज्ञ (इष्टि) की रक्षा के लिए राम को अपने साथ ले जाने विश्वामित्र एक दिन अचानक दशरथ के पास आ पहुँचते हैं। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा संपन्न होते ही मिथिला के राजा जनक द्वारा अनुष्ठित धर्नुयर्ज्ञ में सम्मिलित होने के लिए विश्वामित्र के साथ उन्हीं के अनुरोध या संकेत पर राम और लक्ष्मण मिथला पहुँचते हैं। इस प्रकार अयोध्या का यज्ञ राम को अवतरित कर देता है तो सिद्धाश्रम का यज्ञ राम को असत् के निराकरण और सत् के संस्थापन के लिए सन्नद्ध बना देता है और मिथिला का यज्ञ दशरथनंदन को सीतापति बना देता है। इस प्रकार बालकांड में तीन विशिष्ट इष्टियों की श्रृंखला दिखाई देती है जिससे अयोध्या के राजपरिवार को तो इष्ट सिद्धि होती ही है, साथ ही, समस्त राम परिवार को इष्ट लाभ भी होता है।
सीता और राम का विवाह भी अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण इष्टि है, क्योंकि सीता-राम का समागम केवल एक साधारण नर नारी का संगम नहीं है, वह धरती और आकाश का मिलन है, सुगंध और माधुर्य का सम्मिश्रण है तो सौंदर्य और सत्य का समेकन है। बालकांड में संपन्न प्रत्येक इष्टि में समष्टि की भावना स्पष्ट दिखाई देती है और यही समष्टि भावना सीता-राम के समागम का भी सत्त्व सार है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book