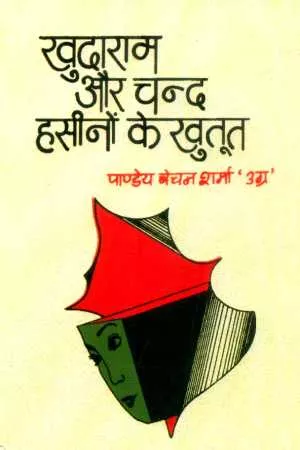|
उपन्यास >> खुदाराम और चन्द हसीनों के खुतूत खुदाराम और चन्द हसीनों के खुतूतपाण्डेय बेचन शर्मा
|
397 पाठक हैं |
|||||||
1927 में लिखी गई इस पुस्तक में हिन्दू-मुसलिम जन-जीवन के आपसी संबंधों की गुत्थियों का मार्मिक विवरण
Alka
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्रकाशकीय
अगर बनारसीदास चतुर्वेदी ने साहित्यिक-युद्ध की नीति को बालाएताक़ रख, मेरी मशहूर पुस्तक ‘चॉकलेट’ पर महात्मा गांधी की राय 25 बरसों तक छिपा न रखी होती, तो मेरी एक भी पुस्तक किसी दूसरे प्रकाशक के हाथ न लगी होती। मेरा दावा यह कि हिन्दी में मेरा ‘केस’ विशेष है। मैं सरकार से पैसा नहीं पाता, न चाहता हूँ; मैं रेडियो पर आज तक कभी बोला नहीं, न चाहता हूँ; दान न तो मैं वैश्य से चाहता हूँ और न वेश्या से: जोड़ बाकी से अपरिचित होने से-इतनी शोहरत होने पर भी-रायल्टी से मेरी आमदनी नहीं के बराबर है। रायल्टी केवल शोहरत से नहीं मिलती, न गुण से;-खुशामद और पैरवी भी ज़रूरी है। ये पंक्तियाँ लिखते समय मेरी अवस्था 54 साल 4 महीने और 4 दिन है। मैं तो ढीठ या निर्लज्ज था क्रूर या ‘उग्र’ होने से अभी तगड़ा हूँ; नहीं तो मेरी अवस्था वाले अनेक मित्र न जाने कभी निज-निज कर्मानुसार नरक या स्वर्ग की राह लग गए ! लेकिन मैं आप ही से पूछूँ कि इस अर्थ-युग में ऐसी आर्थिक-दुर्वस्था में मेरे-जैसा कटु-कषाय ‘उग्र’ यदि कुछ दिनों के लिए-ख़ुदा न करे !-बीमार पड़ जाय क़लम घिसकर चना-चबेना जुटाने में असमर्थ हो जाय, तो क्या होगा ? मेरे स्त्री नहीं पुत्र नहीं, गुरुडम विरोधी होने से शिष्य नहीं, मित्र नहीं, रायल्टी नहीं, घर नहीं, ज़मीन नहीं। और सारी ज़िन्दगी मैं उग्र रहा-अकड़कर चलनेवाला पहाड़ी-मिर्ज़ापुरी।
अस्तु अब सिवा इसके कि मैं अपनी सारी पुस्तकें स्वयं छाप लूँ और बिक्री का प्रबन्ध करूँ मेरे लिए दूसरा कोई चारा नहीं। कापीराइट क़ानून में जल्द ही लेखकों के पक्ष में सुधार-संशोधन भी होने के लक्षण स्पष्ट हैं; पर, तब तक प्रतीक्षा करने जितनी पूंजी मेरे पास नहीं। सत्यतः सारी ज़िन्दगी की कमाई आज से 30 बरस पहले ही कर लेने के बावजूद अन्तिम काल में लाल पैसे भी मुहाल देख मुझे अपनी रचनाओं के छापने का सहज निश्चय करना पड़ा। क्योंकि समाज वादी व्यवस्था के सूर्योदय में जैसे खेत उसका जो जोते, घर उसका जो रहे, कारख़ाने उनके जो परिश्रम करें वैसे ही, पुस्तकें भी उसी की जो उनका लेखक है। समय आने पर, इस मसले पर, मैं समाज संरक्षकों और सरकार की राय या व्यवस्था सहर्ष जानना चाहूँगा।
‘चन्द्र हसीनों के खुतूत’ सन् 1927 ई. में कलकत्ते के ‘मतवाला’ में जैसा कुछ प्रकाशित हुआ था अथवा उसके प्रारम्भिक संस्करणों का जो पाठ था, वह दूसरे प्रकाशक के यहाँ से छपने पर न रह सका। तपते हुए अंग्रेज़ों के भय से उनके शासन के विरुद्ध किए गये अनेक उग्र-इशारे नहीं छापे गये। अब पुस्तक के इस 8 वें संस्करण में दो-चार शब्द मैंने स्वयं बदल दिए या हल्ले कर दिए हैं, जिनका सम्बन्ध हमारे मुस्लिम भाइयों से था। याद रहे, यह उपन्यास सन् 1927 में लिखा गया था, याने पाकिस्तान के जन्म से बीसों बरस पहले। तब और आज की उपस्थित समस्याओं में ज़मीन आसमान का अन्तर हो सकता है।
‘चन्द हसीनों के खुतूत’ विश्व के उपन्यास-साहित्य में हर्गिज़ नाम लेने क़ाबिल नहीं, मगर, हिन्दी में इसने मुझे बहुत यश दिया। आदमी बिल्कुल घोंघावसन्त न हो तो, निश्चय ही यश या पब्लिसिटी पैसे बन-कर रहती है। ‘चन्द हसीनों के ख़ुतूत’ से जो मुझे शोहरत मिली उससे मैं मालामाल हो गया और अब, भले ही मेरी जेब में एक टका न हो, पर धन मेरे चारों ओर गुजराती गरबा नाचता रहता है। फिर भी, हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्ध-सुधार पर आज मुझे लिखना हो, तो कुछ भी न क्यों लिखूं पर ‘चन्द हसीनों के ख़ूतूत’ तो हर्गिज नहीं लिखूँगा। मेरी बुद्धि बदल गई; सो बात नहीं-काल बदल गया, वक्त बदल गया।
पुस्तकों का कम दाम रखने की ज़रूरत महसूस करते हुए भी मैं बाज़ार भाव के अनुसार दाम रखने के लिए लज्जित-लाचार हूँ। बेचने का अपना साधन न हो तो, सस्ती पुस्तकें छापनेवाला-अधिक कमीशन देने में असमर्थ-मर ही जाएगा। एक बात और भी विचित्र है। पुस्तक मौलिक हो या अनुवाद, लेखक कालिदास हों या कवि कल्लू-टके सेर भाजी टके सेर खाजा-सभी की पुस्तकों का मूल्य चार आने फ़र्मे की दर से निर्धारित ! जिस समय ‘उग्र’ ने प्रकाशक बनने का दृढ़ निश्चिय किया उस समय हिन्दी प्रकाशन जगत में स्वराज्य के बाद की अराजकता बहुरंग विराज रही थी।
इसी संग्रह की कहानी ‘ख़ुदाराम’ आज से 31 बरस पहले प्रकाशित हुई थी और लघु उपन्यास ‘चन्द हसीनों के ख़ुतूत’ ने 28 बरस पहले हिंदी साहित्य में कोलाहल पैदा किया था। ‘खुदाराम’ और ‘चन्द हसीनों के ख़ुतूत के साथ ही उग्र-प्रकाशन की तीसरी पुस्तक कढ़ी में कोयला’ भी प्रकाशित हुई है। इस उपन्यास में कलकत्ते के भयंकर रहस्यों भरे जीवन पर सरस, मगर तीव्र प्रकाश डाला गया है। ‘कढ़ी में कोयला’ ‘उग्र लिखित ताज़ातम उपन्यास है।
जय माता की !
अस्तु अब सिवा इसके कि मैं अपनी सारी पुस्तकें स्वयं छाप लूँ और बिक्री का प्रबन्ध करूँ मेरे लिए दूसरा कोई चारा नहीं। कापीराइट क़ानून में जल्द ही लेखकों के पक्ष में सुधार-संशोधन भी होने के लक्षण स्पष्ट हैं; पर, तब तक प्रतीक्षा करने जितनी पूंजी मेरे पास नहीं। सत्यतः सारी ज़िन्दगी की कमाई आज से 30 बरस पहले ही कर लेने के बावजूद अन्तिम काल में लाल पैसे भी मुहाल देख मुझे अपनी रचनाओं के छापने का सहज निश्चय करना पड़ा। क्योंकि समाज वादी व्यवस्था के सूर्योदय में जैसे खेत उसका जो जोते, घर उसका जो रहे, कारख़ाने उनके जो परिश्रम करें वैसे ही, पुस्तकें भी उसी की जो उनका लेखक है। समय आने पर, इस मसले पर, मैं समाज संरक्षकों और सरकार की राय या व्यवस्था सहर्ष जानना चाहूँगा।
‘चन्द्र हसीनों के खुतूत’ सन् 1927 ई. में कलकत्ते के ‘मतवाला’ में जैसा कुछ प्रकाशित हुआ था अथवा उसके प्रारम्भिक संस्करणों का जो पाठ था, वह दूसरे प्रकाशक के यहाँ से छपने पर न रह सका। तपते हुए अंग्रेज़ों के भय से उनके शासन के विरुद्ध किए गये अनेक उग्र-इशारे नहीं छापे गये। अब पुस्तक के इस 8 वें संस्करण में दो-चार शब्द मैंने स्वयं बदल दिए या हल्ले कर दिए हैं, जिनका सम्बन्ध हमारे मुस्लिम भाइयों से था। याद रहे, यह उपन्यास सन् 1927 में लिखा गया था, याने पाकिस्तान के जन्म से बीसों बरस पहले। तब और आज की उपस्थित समस्याओं में ज़मीन आसमान का अन्तर हो सकता है।
‘चन्द हसीनों के खुतूत’ विश्व के उपन्यास-साहित्य में हर्गिज़ नाम लेने क़ाबिल नहीं, मगर, हिन्दी में इसने मुझे बहुत यश दिया। आदमी बिल्कुल घोंघावसन्त न हो तो, निश्चय ही यश या पब्लिसिटी पैसे बन-कर रहती है। ‘चन्द हसीनों के ख़ुतूत’ से जो मुझे शोहरत मिली उससे मैं मालामाल हो गया और अब, भले ही मेरी जेब में एक टका न हो, पर धन मेरे चारों ओर गुजराती गरबा नाचता रहता है। फिर भी, हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्ध-सुधार पर आज मुझे लिखना हो, तो कुछ भी न क्यों लिखूं पर ‘चन्द हसीनों के ख़ूतूत’ तो हर्गिज नहीं लिखूँगा। मेरी बुद्धि बदल गई; सो बात नहीं-काल बदल गया, वक्त बदल गया।
पुस्तकों का कम दाम रखने की ज़रूरत महसूस करते हुए भी मैं बाज़ार भाव के अनुसार दाम रखने के लिए लज्जित-लाचार हूँ। बेचने का अपना साधन न हो तो, सस्ती पुस्तकें छापनेवाला-अधिक कमीशन देने में असमर्थ-मर ही जाएगा। एक बात और भी विचित्र है। पुस्तक मौलिक हो या अनुवाद, लेखक कालिदास हों या कवि कल्लू-टके सेर भाजी टके सेर खाजा-सभी की पुस्तकों का मूल्य चार आने फ़र्मे की दर से निर्धारित ! जिस समय ‘उग्र’ ने प्रकाशक बनने का दृढ़ निश्चिय किया उस समय हिन्दी प्रकाशन जगत में स्वराज्य के बाद की अराजकता बहुरंग विराज रही थी।
इसी संग्रह की कहानी ‘ख़ुदाराम’ आज से 31 बरस पहले प्रकाशित हुई थी और लघु उपन्यास ‘चन्द हसीनों के ख़ुतूत’ ने 28 बरस पहले हिंदी साहित्य में कोलाहल पैदा किया था। ‘खुदाराम’ और ‘चन्द हसीनों के ख़ुतूत के साथ ही उग्र-प्रकाशन की तीसरी पुस्तक कढ़ी में कोयला’ भी प्रकाशित हुई है। इस उपन्यास में कलकत्ते के भयंकर रहस्यों भरे जीवन पर सरस, मगर तीव्र प्रकाश डाला गया है। ‘कढ़ी में कोयला’ ‘उग्र लिखित ताज़ातम उपन्यास है।
जय माता की !
‘उग्र’ प्रकाशन
सदर बाजार, दिल्ली 1-6-55
सदर बाजार, दिल्ली 1-6-55
-पाण्डेय बेचन शर्मा ‘उग्र’
-----------------------
इस पुस्तक को स्वयं प्रकाशित करते समय ये पंक्तियाँ उग्रजी ने लिखी थीं। ये हम यहाँ यथावत प्रकाशित कर रहे हैं।
इस पुस्तक को स्वयं प्रकाशित करते समय ये पंक्तियाँ उग्रजी ने लिखी थीं। ये हम यहाँ यथावत प्रकाशित कर रहे हैं।
खुदाराम
हमारे क़स्बे के इनायत अली कल तक नौमुसलिम थे। उनका परिवार केवल सात वर्षों से ख़ुदा के आगे घुटने टेक रहा था। इसके पहले उनके सिर पर भी चोटी थी, माथे पर तिलक था और घर में ठाकुरजी थे। हमारे समाज ने उनके निरपराध परिवार को ज़बरदस्ती मन्दिर से ढकेलकर मस्जिद में भेज दिया था।
बात यों थी। इनायत अली के बाप उल्फ़त अली जब हिन्दू थे, देवनन्दन प्रसाद थे, तब उनसे अनजाने में एक अपराध बन पड़ा था। एक दिन एक दुखिया ग़रीब युवती ने उनके घर आकर आश्रय माँगा। पता-ठिकाना पूछने पर उसने एक गाँव का नाम ले लिया। कहा-
‘मैं बिलकुल अनाथ हूँ। मेरे मालिक को गुजरे छः महीने से ऊपर हो गये। जब तक वह थे, मुझे कोई फ़िक्र न थी। ज़मींदार की नौकरी से चार पैसे पैदा करके, वही हमारी दुनिया चलाते थे। उनके वक्त ग़रीब होने पर भी मैं किसी की चाकरी नहीं करती थी। अब उनके बाद, उसी गाँव में, पेट के लिए परदा छोड़ते मुझे शर्म मालूम होने लगी। इसीलिए उस गाँव को छोड़ इस शहर में नौकरी तलाश रही हूँ। मुझे और कुछ नहीं, चार रोटियाँ और चार गज कपड़े की जरूरत है। आपको भगवान ने चार पैसे दिए हैं। मेरी हालत पर रहम कीजिये। मुझे अपने घर के एक कोने में रहने और बाक़ी ज़िन्दगी ईश्वर का नाम लेने में बिताने दीजिए। आपका भला होगा।’’
जात पूछने पर उसने अपने को अहीरन बताया। देवनन्दन प्रसादजी सरल हृदय के थे। स्त्री की हालत पर दया आ गई। उनकी स्त्री ने भी अहीरन की मदद ही की। कहा-
‘‘रख लो न। चौका बर्तन किया करेगी, पानी भरेगी, दो रोटी खायगी और पड़ी रहेगी।’’
अहीरन रख ली गई। दो महीनों तक वह घर का काम-काज सँभालती रही। इसके बाद एक दिन एकाएक वज्रपात हुआ। न जाने कहाँ से ढूँढता-ढ़ूँढ़ता एक आदमी देवनन्दनजी के यहाँ आया। पूछने लगा-‘‘बाबूजी, आपने कोई नई मज़दूरन रखी है ?’’
‘‘क्यों भाई ? तुम्हारे इस सवाल का क्या मतलब है ?’’
‘‘बाबूजी, दो महीनों से मेरी औरत लापता है। मैं उसी की तलाश में चारों ओर की खाक छान रहा हूँ। ज़रा-सी बात पर लड़कर भाग खड़ी हुई। औरत की जात, अपने हठ के आगे मर्द की इज्ज़त को कुछ समझती ही नहीं।’’
इसी समय हाथ में घड़ा और रस्सी लिये वह अहीरन घर से बाहर निकली। उसे देखते ही वह पुरुष झपटकर उसके पास पहुँचा।
‘‘अरे, फ़िरोजी ! यह क्या ? किसके लिए पानी भरने जा रही है।’’
‘‘इधर आओ जी !’’ ज़रा कड़े होकर देवनन्दनजी ने कहा-‘‘यह कैसा पागलपन है ? तुम किसे फ़िरोज़ी कह रहे हो ? वह हमारी मजदूरिन है। हमारे लिए पानी लेने जा रही है। उसका नाम फ़िरोज़ी नहीं रुकमिनियाँ है। किसी ग़ैर औरत का इस तरह अपमान करते तुम्हें शर्म नहीं आती ?’’
जोश में देवनन्दनजी इतना कह तो गए, मगर, रुकमिनियाँ के चेहरे पर नजर पड़ते ही उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उस पुरुष को देखते ही अहीरन रुकमिनियाँ का मुँह काला पड़ गया। वह काठमारीसी जहाँ-की-तहाँ खड़ी रह गई।
रुकमिनियाँ को फ़िरोज़ी कहने वाले ने देवनन्दन की ओर देखकर कहा-
‘‘बाबूजी, आपने धोका खाया। यह हिन्दू नहीं, मुसलमान है। रुकमिनियाँ नहीं, मेरी भागी हुई बीबी फ़िरोज़ी है।’’
देवनन्दन के काटो तो खून नहीं !
बात यों थी। इनायत अली के बाप उल्फ़त अली जब हिन्दू थे, देवनन्दन प्रसाद थे, तब उनसे अनजाने में एक अपराध बन पड़ा था। एक दिन एक दुखिया ग़रीब युवती ने उनके घर आकर आश्रय माँगा। पता-ठिकाना पूछने पर उसने एक गाँव का नाम ले लिया। कहा-
‘मैं बिलकुल अनाथ हूँ। मेरे मालिक को गुजरे छः महीने से ऊपर हो गये। जब तक वह थे, मुझे कोई फ़िक्र न थी। ज़मींदार की नौकरी से चार पैसे पैदा करके, वही हमारी दुनिया चलाते थे। उनके वक्त ग़रीब होने पर भी मैं किसी की चाकरी नहीं करती थी। अब उनके बाद, उसी गाँव में, पेट के लिए परदा छोड़ते मुझे शर्म मालूम होने लगी। इसीलिए उस गाँव को छोड़ इस शहर में नौकरी तलाश रही हूँ। मुझे और कुछ नहीं, चार रोटियाँ और चार गज कपड़े की जरूरत है। आपको भगवान ने चार पैसे दिए हैं। मेरी हालत पर रहम कीजिये। मुझे अपने घर के एक कोने में रहने और बाक़ी ज़िन्दगी ईश्वर का नाम लेने में बिताने दीजिए। आपका भला होगा।’’
जात पूछने पर उसने अपने को अहीरन बताया। देवनन्दन प्रसादजी सरल हृदय के थे। स्त्री की हालत पर दया आ गई। उनकी स्त्री ने भी अहीरन की मदद ही की। कहा-
‘‘रख लो न। चौका बर्तन किया करेगी, पानी भरेगी, दो रोटी खायगी और पड़ी रहेगी।’’
अहीरन रख ली गई। दो महीनों तक वह घर का काम-काज सँभालती रही। इसके बाद एक दिन एकाएक वज्रपात हुआ। न जाने कहाँ से ढूँढता-ढ़ूँढ़ता एक आदमी देवनन्दनजी के यहाँ आया। पूछने लगा-‘‘बाबूजी, आपने कोई नई मज़दूरन रखी है ?’’
‘‘क्यों भाई ? तुम्हारे इस सवाल का क्या मतलब है ?’’
‘‘बाबूजी, दो महीनों से मेरी औरत लापता है। मैं उसी की तलाश में चारों ओर की खाक छान रहा हूँ। ज़रा-सी बात पर लड़कर भाग खड़ी हुई। औरत की जात, अपने हठ के आगे मर्द की इज्ज़त को कुछ समझती ही नहीं।’’
इसी समय हाथ में घड़ा और रस्सी लिये वह अहीरन घर से बाहर निकली। उसे देखते ही वह पुरुष झपटकर उसके पास पहुँचा।
‘‘अरे, फ़िरोजी ! यह क्या ? किसके लिए पानी भरने जा रही है।’’
‘‘इधर आओ जी !’’ ज़रा कड़े होकर देवनन्दनजी ने कहा-‘‘यह कैसा पागलपन है ? तुम किसे फ़िरोज़ी कह रहे हो ? वह हमारी मजदूरिन है। हमारे लिए पानी लेने जा रही है। उसका नाम फ़िरोज़ी नहीं रुकमिनियाँ है। किसी ग़ैर औरत का इस तरह अपमान करते तुम्हें शर्म नहीं आती ?’’
जोश में देवनन्दनजी इतना कह तो गए, मगर, रुकमिनियाँ के चेहरे पर नजर पड़ते ही उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उस पुरुष को देखते ही अहीरन रुकमिनियाँ का मुँह काला पड़ गया। वह काठमारीसी जहाँ-की-तहाँ खड़ी रह गई।
रुकमिनियाँ को फ़िरोज़ी कहने वाले ने देवनन्दन की ओर देखकर कहा-
‘‘बाबूजी, आपने धोका खाया। यह हिन्दू नहीं, मुसलमान है। रुकमिनियाँ नहीं, मेरी भागी हुई बीबी फ़िरोज़ी है।’’
देवनन्दन के काटो तो खून नहीं !
2
शाम को, घर के सरदारों के घूमने-फिरने, मिलने-जुलने के लिए निकल जाने का बाद मुहल्ले की बूढ़ी औरतें और जवान लड़कियाँ अपने-अपने दरवाजों पर बैठकर जोर-ज़ोर से देवनन्दन और फ़िरोजी की चर्चा करने लगीं।
‘बाबा रे बाबा !’’ एक बूढ़ी ने राग अलापा-‘‘औरत का ऐसा दीदा ! मर्द को छोड़कर दूसरे देश और दूसरे के घर पर चली आई !’’
‘‘मू-झौंसी थी तो तुर्किन, बन गई अहीरिन। मुसलमान औरतों में लाज नहीं होती, माँ। वह तो इस तरह अपने मालिक को छोड़कर दूसरों के यहाँ चली आई; मुझे तो घर के भी बाहर जाने में डर मालूम होता है। निगोड़ी औरत क्या थी, पतुरिया थी।’’ एक विवाहित लड़की ने कहा।
सामने के दरवाजे पर से दूसरी अधेड़ औरत ने कहा-
‘‘अब देखो रघुनन्दन के बाप का क्या होता है। दो महीनों तक तुर्किन के हाथ का पानी पीकर और उससे चौका-बर्तन कराकर उन्होंने अपना धरम खो दिया है। हमारे...तो कह रहे थे कि अब उनके घर से कोई नाता न रखा जाएगा।’’
‘‘नाता कैसे रखा जा सकता है ?’’ पहली बूढ़ी ने कहा, ‘‘धरम तो कच्चा सूत होता है। ज़रा-सा इधर-उधर होते ही टूट जाता है। फिर हमारा हिन्दू का धरम। राम, राम। जिसको छूना मना है, सुबह जिसका मुँह देखना पाप है, उसके हाथ से देवनन्दन ने जल ग्रहण किया। डूब गया-देवनन्दन का खानदान डूब गया। अब उनसे पान-पानी का नाता रख कौन अपना लोक-परलोक बिगाड़ेगा ?’’
विवाहिता लड़की बोली-
‘‘यह बात शहर भर में फैल गई होगी। दो-चार आदमी जानते होते तो छिपाते भी। सुबह उस तुर्किन का आदमी चोटी पकड़कर धों-धों पीटता हुआ उसे ले जा रहा था। सबने देखा, सब जान गए।’’
बस। दूसरे दिन मुहल्ले के मुखिया ने देवनन्दन को बुलाकर कहा-
‘‘देखो भाई, अब तुम अपने लिए किसी दूसरे कुएँ से पानी मँगाया करो।’’
‘‘क्यों ?’’
‘‘तुम अब हिन्दू नहीं, मुसलमान हो। दो महीने तक मुसलमानिन से पानी भराने और चौका-बर्तन कराने के बाद भी तुम्हारा हिन्दू रहना असम्भव है।’’
‘‘मैंने कुछ जान-बूझकर तो मुसलमानिन के हाथ का पानी पिया नहीं। उसने मुझे धोखा दिया। इसमें मेरा क्या अपराध हो सकता है ?’’
‘‘भैया मेरे, हम हिन्दू हैं। कोई जान-बूझकर गो-हत्या करने के लिए गाय के गले में रस्सी नहीं बाँधता। फिर भी, बँधी हुई गाय के मरने पर बाँधने वाले को हत्या लगती है। प्रायश्चित करना पड़ता है।’’
‘‘यह ठीक है। उसके जाने के बाद ही मैंने तमाम मकान साफ कराया-लिपाया पुताया है मिट्टी के बर्तन बदलवा दिए हैं। धातु के बर्तनों को आग से शुद्ध कर लिया है। इस पर भी और जो कुछ प्रायश्चित कराना हो करा लो। मैं कहीं भागा तो जा नहीं रहा हूँ।’’
प्रायश्चित की चर्चा चलने पर व्यवस्था के लिए पुरोहित और पंडितों की पुकार हुई। बस, ब्राह्मणों ने चारों वेद, छःहो शास्त्र, छत्तीसो स्मृति और अट्ठारहो पुराण का मत लेकर यह व्यवस्था दी कि ‘‘अब, देवनन्दन पूरे म्लेच्छ हो गए। यह किसी तरह भी हिन्दू नहीं हो सकते।’’
उधर देवनन्दन की दुर्दशा का हाल सुनकर मुसलमानों ने बड़ी प्रसन्नता से अपनी छाती खोल दी। क़स्बे के सभी प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित मुसलमानों ने देवनन्दन को अपनी ओर बड़े प्रेम, बड़े आदर से खींचा।
‘‘चलो आओ ! हम जात-पात नहीं, केवल हक़ को मानते हैं। इस्लाम में मुहब्बत भरी हुई है। ख़ुदा ग़रीबपरवर है। हिन्दुओं की ठोकर खाने से अच्छा है कि हमारी पलकों पर बैठो-मुसलमान हो जाओ !’’
लाचार समाज से अपमानित परित्यक्त, पतित देवनन्दन सपरिवार अल्लामियाँ की शरण में चले गये। वह और करते ही क्या ? मनुष्य स्वभाव से ही समाज चाहता है, सहानुभूति चाहता है, प्रेम चाहता है। हिन्दू समाज ने इन सब दरवाजों को देवनन्दन के लिए बन्द कर दिया। इतना हो जाने पर उनके लिए मुसलमान होने के सिवा दूसरा कोई पथ ही नहीं था। देवनन्दन, उल्फ़त अली बन गये और उनका पुत्र रघुनन्दन इनायत अली।
देवनन्दन की छाती पर समाज ने ऐसा क्रूर धक्का मारा कि धर्म-परिवर्तन के नौ महीने बाद ही वे इस दुनिया से कूच कर गये !
‘बाबा रे बाबा !’’ एक बूढ़ी ने राग अलापा-‘‘औरत का ऐसा दीदा ! मर्द को छोड़कर दूसरे देश और दूसरे के घर पर चली आई !’’
‘‘मू-झौंसी थी तो तुर्किन, बन गई अहीरिन। मुसलमान औरतों में लाज नहीं होती, माँ। वह तो इस तरह अपने मालिक को छोड़कर दूसरों के यहाँ चली आई; मुझे तो घर के भी बाहर जाने में डर मालूम होता है। निगोड़ी औरत क्या थी, पतुरिया थी।’’ एक विवाहित लड़की ने कहा।
सामने के दरवाजे पर से दूसरी अधेड़ औरत ने कहा-
‘‘अब देखो रघुनन्दन के बाप का क्या होता है। दो महीनों तक तुर्किन के हाथ का पानी पीकर और उससे चौका-बर्तन कराकर उन्होंने अपना धरम खो दिया है। हमारे...तो कह रहे थे कि अब उनके घर से कोई नाता न रखा जाएगा।’’
‘‘नाता कैसे रखा जा सकता है ?’’ पहली बूढ़ी ने कहा, ‘‘धरम तो कच्चा सूत होता है। ज़रा-सा इधर-उधर होते ही टूट जाता है। फिर हमारा हिन्दू का धरम। राम, राम। जिसको छूना मना है, सुबह जिसका मुँह देखना पाप है, उसके हाथ से देवनन्दन ने जल ग्रहण किया। डूब गया-देवनन्दन का खानदान डूब गया। अब उनसे पान-पानी का नाता रख कौन अपना लोक-परलोक बिगाड़ेगा ?’’
विवाहिता लड़की बोली-
‘‘यह बात शहर भर में फैल गई होगी। दो-चार आदमी जानते होते तो छिपाते भी। सुबह उस तुर्किन का आदमी चोटी पकड़कर धों-धों पीटता हुआ उसे ले जा रहा था। सबने देखा, सब जान गए।’’
बस। दूसरे दिन मुहल्ले के मुखिया ने देवनन्दन को बुलाकर कहा-
‘‘देखो भाई, अब तुम अपने लिए किसी दूसरे कुएँ से पानी मँगाया करो।’’
‘‘क्यों ?’’
‘‘तुम अब हिन्दू नहीं, मुसलमान हो। दो महीने तक मुसलमानिन से पानी भराने और चौका-बर्तन कराने के बाद भी तुम्हारा हिन्दू रहना असम्भव है।’’
‘‘मैंने कुछ जान-बूझकर तो मुसलमानिन के हाथ का पानी पिया नहीं। उसने मुझे धोखा दिया। इसमें मेरा क्या अपराध हो सकता है ?’’
‘‘भैया मेरे, हम हिन्दू हैं। कोई जान-बूझकर गो-हत्या करने के लिए गाय के गले में रस्सी नहीं बाँधता। फिर भी, बँधी हुई गाय के मरने पर बाँधने वाले को हत्या लगती है। प्रायश्चित करना पड़ता है।’’
‘‘यह ठीक है। उसके जाने के बाद ही मैंने तमाम मकान साफ कराया-लिपाया पुताया है मिट्टी के बर्तन बदलवा दिए हैं। धातु के बर्तनों को आग से शुद्ध कर लिया है। इस पर भी और जो कुछ प्रायश्चित कराना हो करा लो। मैं कहीं भागा तो जा नहीं रहा हूँ।’’
प्रायश्चित की चर्चा चलने पर व्यवस्था के लिए पुरोहित और पंडितों की पुकार हुई। बस, ब्राह्मणों ने चारों वेद, छःहो शास्त्र, छत्तीसो स्मृति और अट्ठारहो पुराण का मत लेकर यह व्यवस्था दी कि ‘‘अब, देवनन्दन पूरे म्लेच्छ हो गए। यह किसी तरह भी हिन्दू नहीं हो सकते।’’
उधर देवनन्दन की दुर्दशा का हाल सुनकर मुसलमानों ने बड़ी प्रसन्नता से अपनी छाती खोल दी। क़स्बे के सभी प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित मुसलमानों ने देवनन्दन को अपनी ओर बड़े प्रेम, बड़े आदर से खींचा।
‘‘चलो आओ ! हम जात-पात नहीं, केवल हक़ को मानते हैं। इस्लाम में मुहब्बत भरी हुई है। ख़ुदा ग़रीबपरवर है। हिन्दुओं की ठोकर खाने से अच्छा है कि हमारी पलकों पर बैठो-मुसलमान हो जाओ !’’
लाचार समाज से अपमानित परित्यक्त, पतित देवनन्दन सपरिवार अल्लामियाँ की शरण में चले गये। वह और करते ही क्या ? मनुष्य स्वभाव से ही समाज चाहता है, सहानुभूति चाहता है, प्रेम चाहता है। हिन्दू समाज ने इन सब दरवाजों को देवनन्दन के लिए बन्द कर दिया। इतना हो जाने पर उनके लिए मुसलमान होने के सिवा दूसरा कोई पथ ही नहीं था। देवनन्दन, उल्फ़त अली बन गये और उनका पुत्र रघुनन्दन इनायत अली।
देवनन्दन की छाती पर समाज ने ऐसा क्रूर धक्का मारा कि धर्म-परिवर्तन के नौ महीने बाद ही वे इस दुनिया से कूच कर गये !
3
जिन दिनों की घटना ऊपर लिखी गई है उन्हें भूत के गर्भ में गये सात वर्ष हो गये। तब से हमारे क़स्बे की हालत अब बहुत कुछ बदल-सी गई है। पहले हमारे यहाँ सामाजिक या राजनीतिक जीवन बिल्कुल नहीं था। सभी पेट के धन्धे की धुन में व्यस्त थे। उन दिनों हमारी दस हजार की बस्ती में, क्लब या सोसायटी के नाते तहसील का अहाता मात्र था, जहाँ नित्य सायंकाल नगर के दस-पाँच चापलूस धनी तहसीलदार से हें-हें करने के लिए या टेनिस खेलने के लिए एकत्र हुआ करते थे। आर्यसमाज का बदनाम नाम तो घर-घर था, मगर, सच्चा आर्यसमाजी एक भी न था। एक सज्जन आगरे के ‘आर्यमित्र’ के ग्राहक थे। वही स्वामी दयानन्द का नाम ले-लेकर कभी-कभी नवयुवकों के विनोद के साधन बना करते थे। वह बनते तो थे आर्यसमाजी मगर बिल्कुल मौखिक। हमें ठीक याद है, वह पुराने समाज की सभी प्रथा या कुप्रथाओं को मानते थे। एक बार उनकी स्त्री ने उनसे सत्यनारायण की कथा सुनने का आग्रह किया और उन्होंने अस्वीकार कर दिया। बस, इसी बात पर आर्यसमाजी पति के मुख पर सनातनी चंडी झाड़ू, फेरने, कालिख लगाने और चूना करने को तैयार हो गई ! तीन दिनों तक मुहल्ले वालों को नींद हराम हो गई। विवश होकर ‘महाशयजी’ को स्त्री के आगे झुकना पड़ा।
मगर, अब क़स्बे का वातावरण बिल्कुल परिवर्तित हो गया है। गत असहयोग आन्दोलन के प्रसाद से हमारा क़स्बा भी बहुत कुछ जीवित हो उठा है। अब हमारे यहाँ बक़ायदा आर्यसमाज भवन है, और हैं उसके मन्त्री, सभापति। एक पुस्तकालय भी है और उसके भी मन्त्री सभापति हैं। हिन्दी के अनेक पत्र और अंग्रेजी के दो-तीन दैनिक आते हैं। सैकड़ों बालक, युवक और वृद्ध अख़बार जीवी बन गये हैं। ऐसे अख़बार-जीवियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।
उस दिन आर्यसमाज के मन्त्री पण्डित वासुदेव शर्मा समाज भवन में बैठे कोई उर्दू अख़बार पढ़ रहे थे। भवन के बाहर-बरामदे में दो पंजाबी ‘महाशय’ पायजामा और कमीज पहने सायं-सन्ध्या कर रहे थे। उसी समय एक, दुबला-पतला लम्बा-सा पुरुष भवन में आया। उसकी आहट पा शर्माजी ने चश्माच्छ आँखों से उसकी ओर देखा। पहचान गये-
‘‘कहो मियाँ इनायत अली, आज इधर कैसे ?’’
‘‘आपही की सेवा में कुछ निवेदन करने आया हूँ।’’
शर्माजी ने चश्मा उतार लिया। उसे कुरते के कोने से साफ़ करने के बाद पुनः नाक पर चढ़ाते-चढ़ाते बोले-
‘‘भाई इनायत, बड़ी शुद्ध हिन्दी बोलते हो ?’’
‘‘जी हाँ शर्माजी, मैं बहुत शुद्ध हिन्दी बोल सकता हूँ। इसका कारण यही है कि मेरी नसों में बहुत शुद्ध हिन्दू रक्त बह रहा है। समाज ने ज़बरदस्ती मेरे पिता को मुसलमान होने के लिये विवश किया, नहीं तो, आज मैं भी उतना ही हिन्दू होता जितने आप या कोई भी दूसरा हिन्दुत्व का अभिमानी। ख़ैर मुझे आपसे कुछ कहना है....!’’
‘‘कहिए, क्या आज्ञा है ?’’
‘‘मैं पुनः हिन्दू होना चाहता हूँ ।’’
‘‘हिन्दू होना ??’’ आश्चर्य से मुख विस्फारित कर शर्माजी ने पूछा।
‘‘जी हाँ। अब मुसलमान रहने में लोक-परलोक दोनों का नाश दिखाई पड़ता है। इसलिए नहीं कि उस धर्म में कोई विशेषता नहीं है, बल्कि इसलिए कि मेरा और मेरे परिवार का हृदय मुसलमान धर्म के योग्य नहीं। अनन्त काल का हिन्दू हृदय-हिन्दू सभ्यता का पक्षपाती शान्त हृदय-मुसलमानी रीति-नीति और सभ्यता का उपयोग करने में बिल्कुल अयोग्य साबित हुआ है। मेरी स्त्री नित्य प्रातःकाल ख़ुदा-ख़ुदा नहीं, राम-राम जपती है। मैं मुसलमान रहकर क्या करूँगा ? मेरी माता गंगा स्नान और बदरिकाश्रम यात्रा के लिए तड़पा करती हैं। मेरा हृदय न तो उन्हें मक्का मदीना का भक्त बनाने की धृष्टता कर सकता है और न वह बन ही सकती हैं। मैं मुसलमान रहकर क्या करूँगा ? मैं स्वयं मसजिद में जाकर हृदय के मालिक को नहीं याद कर सकता। मेरा हिन्दू हृदय मस्जिद के द्वार पर पहुँचते ही एक विचित्र स्पन्दन करने लगता है। उस स्पन्दन का अर्थ ख़ुदा या मस्जिद वाले के प्रति अनुराग नहीं हो सकता, घृणा भी नहीं हो सकती। वह स्पन्दन अनुराग और घृणा के मध्य का निवासी है। इन्हीं सब कारणों से, बहुत सोच समझकर अब मैंने शुद्ध होकर हिन्दू होने का निश्चय किया है।’’
पंजाबी महाशय भी सन्ध्या समाप्त कर ओम् ओम् करते हुए भीतर आ गए। शर्माजी ने इनायत अली उर्फ रघुनन्दन का परिचय देते हुए उनके प्रस्ताव पर उन दोनों महाशयों की सम्मति माँगी। ‘‘धन्य हो महाशय जी !’’ एक महाशय बोले-‘‘ऋषि दयानन्द की किरपा होती तो हमारे वे सब बिछड़े भाई एक-न-एक दिन फिर अपने कार्य धरम में चले आएँगे। इन्हें ज़रूर शुद्ध कीजिए।’’
मगर, अब क़स्बे का वातावरण बिल्कुल परिवर्तित हो गया है। गत असहयोग आन्दोलन के प्रसाद से हमारा क़स्बा भी बहुत कुछ जीवित हो उठा है। अब हमारे यहाँ बक़ायदा आर्यसमाज भवन है, और हैं उसके मन्त्री, सभापति। एक पुस्तकालय भी है और उसके भी मन्त्री सभापति हैं। हिन्दी के अनेक पत्र और अंग्रेजी के दो-तीन दैनिक आते हैं। सैकड़ों बालक, युवक और वृद्ध अख़बार जीवी बन गये हैं। ऐसे अख़बार-जीवियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।
उस दिन आर्यसमाज के मन्त्री पण्डित वासुदेव शर्मा समाज भवन में बैठे कोई उर्दू अख़बार पढ़ रहे थे। भवन के बाहर-बरामदे में दो पंजाबी ‘महाशय’ पायजामा और कमीज पहने सायं-सन्ध्या कर रहे थे। उसी समय एक, दुबला-पतला लम्बा-सा पुरुष भवन में आया। उसकी आहट पा शर्माजी ने चश्माच्छ आँखों से उसकी ओर देखा। पहचान गये-
‘‘कहो मियाँ इनायत अली, आज इधर कैसे ?’’
‘‘आपही की सेवा में कुछ निवेदन करने आया हूँ।’’
शर्माजी ने चश्मा उतार लिया। उसे कुरते के कोने से साफ़ करने के बाद पुनः नाक पर चढ़ाते-चढ़ाते बोले-
‘‘भाई इनायत, बड़ी शुद्ध हिन्दी बोलते हो ?’’
‘‘जी हाँ शर्माजी, मैं बहुत शुद्ध हिन्दी बोल सकता हूँ। इसका कारण यही है कि मेरी नसों में बहुत शुद्ध हिन्दू रक्त बह रहा है। समाज ने ज़बरदस्ती मेरे पिता को मुसलमान होने के लिये विवश किया, नहीं तो, आज मैं भी उतना ही हिन्दू होता जितने आप या कोई भी दूसरा हिन्दुत्व का अभिमानी। ख़ैर मुझे आपसे कुछ कहना है....!’’
‘‘कहिए, क्या आज्ञा है ?’’
‘‘मैं पुनः हिन्दू होना चाहता हूँ ।’’
‘‘हिन्दू होना ??’’ आश्चर्य से मुख विस्फारित कर शर्माजी ने पूछा।
‘‘जी हाँ। अब मुसलमान रहने में लोक-परलोक दोनों का नाश दिखाई पड़ता है। इसलिए नहीं कि उस धर्म में कोई विशेषता नहीं है, बल्कि इसलिए कि मेरा और मेरे परिवार का हृदय मुसलमान धर्म के योग्य नहीं। अनन्त काल का हिन्दू हृदय-हिन्दू सभ्यता का पक्षपाती शान्त हृदय-मुसलमानी रीति-नीति और सभ्यता का उपयोग करने में बिल्कुल अयोग्य साबित हुआ है। मेरी स्त्री नित्य प्रातःकाल ख़ुदा-ख़ुदा नहीं, राम-राम जपती है। मैं मुसलमान रहकर क्या करूँगा ? मेरी माता गंगा स्नान और बदरिकाश्रम यात्रा के लिए तड़पा करती हैं। मेरा हृदय न तो उन्हें मक्का मदीना का भक्त बनाने की धृष्टता कर सकता है और न वह बन ही सकती हैं। मैं मुसलमान रहकर क्या करूँगा ? मैं स्वयं मसजिद में जाकर हृदय के मालिक को नहीं याद कर सकता। मेरा हिन्दू हृदय मस्जिद के द्वार पर पहुँचते ही एक विचित्र स्पन्दन करने लगता है। उस स्पन्दन का अर्थ ख़ुदा या मस्जिद वाले के प्रति अनुराग नहीं हो सकता, घृणा भी नहीं हो सकती। वह स्पन्दन अनुराग और घृणा के मध्य का निवासी है। इन्हीं सब कारणों से, बहुत सोच समझकर अब मैंने शुद्ध होकर हिन्दू होने का निश्चय किया है।’’
पंजाबी महाशय भी सन्ध्या समाप्त कर ओम् ओम् करते हुए भीतर आ गए। शर्माजी ने इनायत अली उर्फ रघुनन्दन का परिचय देते हुए उनके प्रस्ताव पर उन दोनों महाशयों की सम्मति माँगी। ‘‘धन्य हो महाशय जी !’’ एक महाशय बोले-‘‘ऋषि दयानन्द की किरपा होती तो हमारे वे सब बिछड़े भाई एक-न-एक दिन फिर अपने कार्य धरम में चले आएँगे। इन्हें ज़रूर शुद्ध कीजिए।’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book