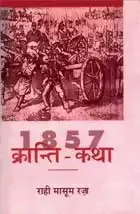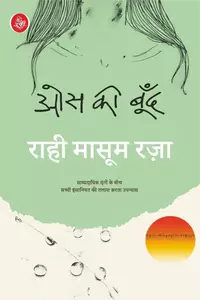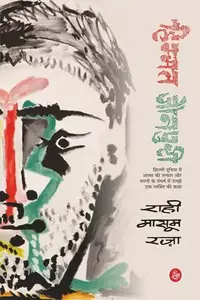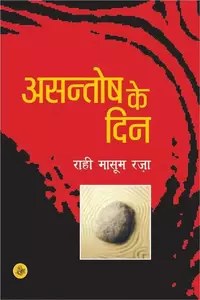|
इतिहास और राजनीति >> 1857-क्रान्ति-कथा 1857-क्रान्ति-कथाराही मासूम रजा
|
3 पाठक हैं |
||||||
1857 की क्रान्ति पर आधारित पुस्तक...
1857 Kranti Katha - Rahi Masoom Raza - 1857 क्रान्ति कथा- राही मासूम रजा
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
इस बात को ताजा करने के लिए हिन्दुस्तानी तवारीख ने मुझे 1857 से बेहतर कोई मिसाल नहीं दी इसलिए मैंने 1857 का इन्तखाब किया। लेकिन 1857 की इस नजम का मौजूं नहीं है। इसका मौंजूं का कोई सन नहीं है इसका मौंजूं इन्सान है। सुकरात जहर पी सकता है, इब्ने मरियम को समलूब किया जा सकता है, ब्रोनो को जिन्दा जलाया जा सकता है, ऐवस्ट की तलाश में कई कारवाँ गुम हो सकते हैं लेकिन सुकरात हारता नहीं, ईसा की शिकस्त नहीं होती, ब्रोनो साबित कदम रखता है और ऐवरेस्ट का गुरूर टूट जाता है। मैंने यह नजम चंद किताबों की मदद से अपने कमरे में बैठकर नहीं लिखी है। मैंने इस लड़ाई की शिरकत की है, मैंने जम लगाये हैं, मैं दरख्त पर लटकाया गया हूँ, मुझे मुर्दा समझकर गिद्धों ने नोचा है। मैंने उस बेबसी को महसूस किया है जब आदमी गिद्धों से और गीदड़ों से बचने के लिए अपना जिस्म नहीं हिला सकता है जब आँखों से बेपनाह खौफ़ बेपनाह बेबसी झलकने लगती है। मैंने उस खौफ को भी महसूस किया है जिसे तोपदम होने से पहले हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने किया होगा। मैंने उस दीवानगी के दिन गुजारे हैं जिसमें चन्द हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने किसी मकान में किलाबन्द होकर अँग्रेजों के लश्कर को रोकने का हौसला किया था।
क्रान्ति-कथा उर्फ अठारह सौ सत्तावन
राही की विचारधारा के विकास का प्रथम सोपान
क्रान्ति-कथा उर्फ 1957 में जब प्रथम स्वाधीनता संग्राम का शताब्दी समारोह मनाया गया उस अवसर पर राही मासूम रज़ा का महाकाव्य ‘अठारह सौ सत्तावन’ प्रकाशित हुआ था। उस समय इतिहासकारों में 1857 के चरित्र को लेकर बहुत विवाद था। बहुत से इतिहासकार उसे सामन्ती व्यवस्था की पुनःस्थापना का आन्दोलन मान रहे थे। उनमें कुछ तो इस सीमा तक बात कर रहे थे कि भारतीय सामन्त अपने खोये हुए राज्यों को प्राप्त करने की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने भारतीय सिपाहियों और किसानों को धार्मिक नारे देकर अपने साथ किया। 1857 के बारे में यह एक सतही और यांत्रिक समझ थी। वास्तव में वह अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय जनता का महासंग्राम था। इस आन्दोलन में किसान और कारीगर अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे थे। इतिहासकार ऐरिक स्टोक ने लिखा है कि मूल किसान भावना कर वसूल करने वालों के विरुद्ध थी। उनसे मुक्ति पाने की थी। चाहे उनका कोई रूप, रंग या राष्ट्रीयता हो। (दि पीजेंट एंड दि राज, कैंब्रिज) जहाँ-जहाँ ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ था, वहाँ सत्ता विद्रोही जमींदारों और किसानों के हाथों में पहुँच गयी। किसान इस सत्ता में बराबर के शरीक थे। इसके साथ ही भारतीय कारीगरों की माँगें भी इस विद्रोह के घोषणा-पत्र में शामिल थीं। अगस्त 1857 के घोषणा-पत्र में विद्रोही राजकुमार फ़िरोजशाह ने स्पष्ट करते हुए कहा था: भारत में अंग्रेजी वस्तुओं को लाकर यूरोप के लोगों ने जुलाहों, दर्जियों, बढ़ई, लुहारों और जूता बनाने वालों को रोजगार से बाहर कर दिया है और उनके पेशों को हड़प लिया है। इस प्रकार प्रत्येक देशी दस्तकार भिखारी की दशा में पहुँच गया है। (एस.ए.ए.रिज्ची: फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तर प्रदेश-1, लखनऊ)
यह सही है कि जब राष्ट्रीय भावना कमजोर होती है तब धार्मिक नारे भी लगाये जाते हैं। अगस्त 57 के घोषणा-पत्र में यह स्पष्ट किया गया था। यह बात सबको अच्छी तरह मालूम है कि हिन्दुस्तान के लोग हिन्दू और मुसलमान दोनों ही काफिर और विश्वासघाती अंग्रेजों के दमन और आतंक से नष्ट हो रहे हैं। क्रान्तिकारियों ने कहा कि हिन्दुस्तान की सारी जनता अंग्रेजों के दमन का शिकार है इसलिए उनसे भारत को मुक्ति दिलाना हर भारतीय का कर्तव्य है।’ (रिज़्वी: फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तर प्रदेश) ये सही है कि विद्रोहियों में उद्देश्यों को लेकर अलग-अलग राय थी लेकिन इसका जनचरित्र भी रेखांकित किया जाना चाहिए। अवध में पुराने राजदरबार की भाषा फ़ारसी की जगह हिन्दुस्तानी का प्रयोग किया गया था जिसमें आमने-सामने उर्दू और हिन्दी दोनों पाठ दिये गये हैं। 6 जुलाई’ 57 को ‘बिरजिस कादर’ नाम से जारी किया गया। यह इश्तहारनामा देश के आम जनता और जमींदारों को सम्बोधित किया गया था जिसमें बहुत सरल भाषा का प्रयोग था और एक सामान्य भाषा की खोज का यह पहला प्रयास है। शायद यह भाषा नीति चलती तो देश में उर्दू-हिन्दी का विवाद न होता। आज धुँधलका साफ है। 1857 के अन्तर्विरोधों से गुजरते हुए इतिहासकार इसे स्वतन्त्रता का पहला संग्राम मान रहे हैं। लेकिन राही के सामने उद्देश्य स्पष्ट थे-यह लड़ाई विदेशी शासकों के विरुद्ध थी। इसे हिन्दू-मुसलमान दोनों मिलकर लड़ रहे थे। इसमें सामन्तों के साथ किसान-मजदूर और कारीगर सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे थे। वे देश में अपना राज्य कायम करना चाहते थे जिसमें वे सम्मान के साथ जी सकें। राही के लिए यह संग्राम भारतीय स्वाभिमान का संघर्ष था। देश की अस्मिता का सवाल था। फिर एक ऐसी सामान्य भाषा 1857 में पैदा हो रही थी जो देश की राजभाषा के रूप में विकसित हो सकती थी। वह जनभाषाओं से भी शब्द चयन कर रही थी। फ़ारसी, संस्कृत, अरबी, हिन्दी-उर्दू का भी इस भाषा के विकास में योगदान था। राही इससे चिन्तित नहीं है कि यदि विद्रोही जीत जाते तो शासन का स्वरूप क्या होता। वे आश्वस्त हैं कि निश्चित ही इसका चरित्र जनविरोधी नहीं होता। भारतीय सामन्तों का वह वर्चस्व नहीं होता जो 1857 से पहले था। राही को देश के भविष्य निर्माण में किसानों, मजदूरों और कारीगरों की भूमिका पर बहुत भरोसा है। राही अक्सर कहते थे कि हिन्दू-मुसलमान यदि देश की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करें तो ये देश सर्वोशिखर पहुँच जाए। 1857 में इस जनएकता से राही बहुत प्रभावित थे। वे सबसे अधिक प्रभावित महिलाओं की भूमिका से थे। पहली बार भारत की स्त्रियों ने अपनी प्रतिभा, त्याग और बलिदान से एक नया इतिहास बनाया। 1857 में उन्होंने खाली बेगम हजरत महल की भूमिका का ही चित्रण नहीं किया है, सबसे अधिक महत्त्व रानी लक्ष्मीबाई तथा उनकी सहयोगी साधारण स्त्रियों को दिया है। ये साधारण स्त्रियाँ अभूतपूर्व संघटन क्षमता, बहादुरी तथा बलिदान का प्रदर्शन करती हैं और उन लोगों पर चोट करती हैं जो स्त्री को द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझते हैं। राही ने अपने महाकाव्य में साधारणजन के साथ इन स्त्रियों के शौर्य और पराक्रम का बहुत जीवन्त चित्रण किया है:
यह सही है कि जब राष्ट्रीय भावना कमजोर होती है तब धार्मिक नारे भी लगाये जाते हैं। अगस्त 57 के घोषणा-पत्र में यह स्पष्ट किया गया था। यह बात सबको अच्छी तरह मालूम है कि हिन्दुस्तान के लोग हिन्दू और मुसलमान दोनों ही काफिर और विश्वासघाती अंग्रेजों के दमन और आतंक से नष्ट हो रहे हैं। क्रान्तिकारियों ने कहा कि हिन्दुस्तान की सारी जनता अंग्रेजों के दमन का शिकार है इसलिए उनसे भारत को मुक्ति दिलाना हर भारतीय का कर्तव्य है।’ (रिज़्वी: फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तर प्रदेश) ये सही है कि विद्रोहियों में उद्देश्यों को लेकर अलग-अलग राय थी लेकिन इसका जनचरित्र भी रेखांकित किया जाना चाहिए। अवध में पुराने राजदरबार की भाषा फ़ारसी की जगह हिन्दुस्तानी का प्रयोग किया गया था जिसमें आमने-सामने उर्दू और हिन्दी दोनों पाठ दिये गये हैं। 6 जुलाई’ 57 को ‘बिरजिस कादर’ नाम से जारी किया गया। यह इश्तहारनामा देश के आम जनता और जमींदारों को सम्बोधित किया गया था जिसमें बहुत सरल भाषा का प्रयोग था और एक सामान्य भाषा की खोज का यह पहला प्रयास है। शायद यह भाषा नीति चलती तो देश में उर्दू-हिन्दी का विवाद न होता। आज धुँधलका साफ है। 1857 के अन्तर्विरोधों से गुजरते हुए इतिहासकार इसे स्वतन्त्रता का पहला संग्राम मान रहे हैं। लेकिन राही के सामने उद्देश्य स्पष्ट थे-यह लड़ाई विदेशी शासकों के विरुद्ध थी। इसे हिन्दू-मुसलमान दोनों मिलकर लड़ रहे थे। इसमें सामन्तों के साथ किसान-मजदूर और कारीगर सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे थे। वे देश में अपना राज्य कायम करना चाहते थे जिसमें वे सम्मान के साथ जी सकें। राही के लिए यह संग्राम भारतीय स्वाभिमान का संघर्ष था। देश की अस्मिता का सवाल था। फिर एक ऐसी सामान्य भाषा 1857 में पैदा हो रही थी जो देश की राजभाषा के रूप में विकसित हो सकती थी। वह जनभाषाओं से भी शब्द चयन कर रही थी। फ़ारसी, संस्कृत, अरबी, हिन्दी-उर्दू का भी इस भाषा के विकास में योगदान था। राही इससे चिन्तित नहीं है कि यदि विद्रोही जीत जाते तो शासन का स्वरूप क्या होता। वे आश्वस्त हैं कि निश्चित ही इसका चरित्र जनविरोधी नहीं होता। भारतीय सामन्तों का वह वर्चस्व नहीं होता जो 1857 से पहले था। राही को देश के भविष्य निर्माण में किसानों, मजदूरों और कारीगरों की भूमिका पर बहुत भरोसा है। राही अक्सर कहते थे कि हिन्दू-मुसलमान यदि देश की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करें तो ये देश सर्वोशिखर पहुँच जाए। 1857 में इस जनएकता से राही बहुत प्रभावित थे। वे सबसे अधिक प्रभावित महिलाओं की भूमिका से थे। पहली बार भारत की स्त्रियों ने अपनी प्रतिभा, त्याग और बलिदान से एक नया इतिहास बनाया। 1857 में उन्होंने खाली बेगम हजरत महल की भूमिका का ही चित्रण नहीं किया है, सबसे अधिक महत्त्व रानी लक्ष्मीबाई तथा उनकी सहयोगी साधारण स्त्रियों को दिया है। ये साधारण स्त्रियाँ अभूतपूर्व संघटन क्षमता, बहादुरी तथा बलिदान का प्रदर्शन करती हैं और उन लोगों पर चोट करती हैं जो स्त्री को द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझते हैं। राही ने अपने महाकाव्य में साधारणजन के साथ इन स्त्रियों के शौर्य और पराक्रम का बहुत जीवन्त चित्रण किया है:
सोचता जा रहा है मुसाफ़िर
गिरती दीवारें फिर बन सकेंगी
थालियाँ खिल-खिलाकर हँसेंगी
पूरियाँ फिर घर में छन सकेंगी।
नाज आयेगा खेतों से घर में
खेत छूटेंगे बनिये के घर से
गीत गाऊँगा उस रह गुजर पर
शर्म आती है जिस रह गुजर से
गिरती दीवारें फिर बन सकेंगी
थालियाँ खिल-खिलाकर हँसेंगी
पूरियाँ फिर घर में छन सकेंगी।
नाज आयेगा खेतों से घर में
खेत छूटेंगे बनिये के घर से
गीत गाऊँगा उस रह गुजर पर
शर्म आती है जिस रह गुजर से
रानी लक्ष्मीबाई पर राही ने अपने महाकाव्य में 40 पृष्ठ लिखे हैं। शायद इतनी लम्बी कविता हिन्दी के किसी कवि ने नहीं लिखी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी के ऊपर एक कविता लिखी जो अत्यन्त लोकप्रिय हुई। राही ने रानी के हर पक्ष का वर्णन किया है।
राही ने यह महाकाव्य 1957 में उर्दू भाषा में लिखा था। उर्दू में तो कोई महाकाव्य है नहीं लेकिन हिन्दी में भी 1857 के महासमर पर कोई इस तरह का महाकाव्य नहीं है, नाटक और उपन्यास तो हैं। 1965 में ये हिन्दी में छपा जिसकी प्रस्तावना प्रसिद्ध विद्वान् डॉ. सम्पूर्णानन्द ने लिखी थी। उन्होंने अप्रैल 1965 में लिखा था कि ‘इस पुस्तक का उद्देश्य है सुनो भाइयो-सुनो भाइयो, कथा सुनो-1857 की। सच तो यह है कि उस उद्देश्य को बहुत अच्छी तरह निभाया गया है। लखनऊ, झाँसी और जहाँ-जहाँ उत्तर प्रदेश के खेत रहे-सबका वर्णन बहुत ही मर्मस्पर्शी शब्दों में किया गया है। मुझे विश्वास है हिन्दी भाषी जगत् इस पुस्तक का समादर करेगा ?’ लेकिन डॉ. सम्पूर्णानन्द की यह आशा हिन्दी जगत् ने निराशा में बदल दी। राही और उसके महाकाव्य की घोर उपेक्षा हुआ। मामूली कवियों को महाकवि सिद्ध किया गया और राही जैसे लोग उपेक्षा के शिकार हुए। आजादी की स्वर्णजयन्ती 1857 के स्वाधीनता संग्राम को स्मरण किए बिना अधूरी है। इस बहाने राही के क्रान्ति-कथा उर्फ ‘अठारह सौ सत्तावन’ को भी याद करना आवश्यक है।
राही ने यह महाकाव्य 1957 में उर्दू भाषा में लिखा था। उर्दू में तो कोई महाकाव्य है नहीं लेकिन हिन्दी में भी 1857 के महासमर पर कोई इस तरह का महाकाव्य नहीं है, नाटक और उपन्यास तो हैं। 1965 में ये हिन्दी में छपा जिसकी प्रस्तावना प्रसिद्ध विद्वान् डॉ. सम्पूर्णानन्द ने लिखी थी। उन्होंने अप्रैल 1965 में लिखा था कि ‘इस पुस्तक का उद्देश्य है सुनो भाइयो-सुनो भाइयो, कथा सुनो-1857 की। सच तो यह है कि उस उद्देश्य को बहुत अच्छी तरह निभाया गया है। लखनऊ, झाँसी और जहाँ-जहाँ उत्तर प्रदेश के खेत रहे-सबका वर्णन बहुत ही मर्मस्पर्शी शब्दों में किया गया है। मुझे विश्वास है हिन्दी भाषी जगत् इस पुस्तक का समादर करेगा ?’ लेकिन डॉ. सम्पूर्णानन्द की यह आशा हिन्दी जगत् ने निराशा में बदल दी। राही और उसके महाकाव्य की घोर उपेक्षा हुआ। मामूली कवियों को महाकवि सिद्ध किया गया और राही जैसे लोग उपेक्षा के शिकार हुए। आजादी की स्वर्णजयन्ती 1857 के स्वाधीनता संग्राम को स्मरण किए बिना अधूरी है। इस बहाने राही के क्रान्ति-कथा उर्फ ‘अठारह सौ सत्तावन’ को भी याद करना आवश्यक है।
कुँवरपाल सिंह
मैंने क्रान्ति-कथा की समरगाथा क्यों लिखी !
असल में शायर ज़िन्दगी का नक़लनवीस नहीं होता कि नुक़ते के मुक़ाबले में नुक़ता और मरकज़ के मुक़ाबले को मरकज़ नकल कर दे, वह तो अपनी हर तख़लीक़ में खुद अपनी शख्सियत का कोई-न-कोई जुज़ मिलता है और यूँ एक ऐसी चीज़ बजूद में आती है जो पहले न थी। शायर नक्क़ाल नहीं होता है-और वह नाक़िद होता है, वह अपनी रद्दोक़बूल से क़दरों की क़ीमत का ताइयुन करता है।
अहम बात सिर्फ यह नहीं होती कि शायर ने किन चीज़ों का इन्तख़ाब किया है। यह बात भी इतनी ही अहम होती है कि उसने किन चीज़ों को इन्तख़ाब नहीं किया है। अगर ये दोनों चीज़ें इसके पेशे-निगाह न हों तो तख़लीक़ एकतरफा होगी इसलिए नाक़िस होगी। शायर को इसका अहसास होना चाहिए कि उसने किसी चीज़ का इन्तख़ाब क्यों नहीं किया। इसी सूरत में वह उन चीज़ों पर जोर दे सकता है जिसका उसने इन्तख़ाब किया है और इसी सूरत में उसे मालूम हो सकता है कि उसे अपनी मुनतसब की हुई चीज़ों पर कहाँ और कितना जोर देना चाहिए।
शायर को यह भी मालूम होना चाहिए कि उसने किसी चीज़ का इन्तख़ाब क्यों किया। उसे मालूम होना चाहिए कि उसने किसी चीज़ के बयान में किसी ख़ास सिनफ़े सुख़न और किसी ख़ास बहर का इन्तख़ाब क्यों किया है। मसनवी क्यों लिखी। मुस्द्दस में क्या बुराई थी, नज़म जिस जगह से शुरू हुई है, उसी जगह से क्यों शुरू हुई है और जहाँ ख़त्म हुई है उसी जगह ख़त्म क्यों हुई। उसे यह तमाम बातें मालूम होनी चाहिए क्योंकि जब वह तख़लीक करता है तो ख़्यालात से आँखमिचौली नहीं खेलता कि जो ख़्याल जहाँ पकड़ गया बस चोर हो गया। शायर शिकारी तो होता नहीं कि लाशऊर की तारीक झील में काँटा फेंककर बैठ जाय कि जो हाथ लग जाय। वह उससे मुतमइन नहीं होता है। शायर तो एक गृहस्थिन की तरह होता है-बाज़ार जाता है, दुकान-दुकान घूमता है, मोलतोल करता है और हर चीज़ नहीं खरीद- लेता है वहीं जीज़ें लेता है जिनकी उसे ज़रूरत होती है और जिन्हें वह ले सकता है। शायरी की बुनियाद शऊर पर होती है लाशऊर पर नहीं-वजदान शायराना लहर और इस क़िस्म की दूसरी इस्तलाहें गुमराहकुन हैं और इन्हें वही शायर इस्तेमाल करते हैं जो अपने मोहरकात से वाक़िफ नहीं होते या जो अपने मोहरकात की निशानदेही से घबराते हैं।
अहम बात सिर्फ यह नहीं होती कि शायर ने किन चीज़ों का इन्तख़ाब किया है। यह बात भी इतनी ही अहम होती है कि उसने किन चीज़ों को इन्तख़ाब नहीं किया है। अगर ये दोनों चीज़ें इसके पेशे-निगाह न हों तो तख़लीक़ एकतरफा होगी इसलिए नाक़िस होगी। शायर को इसका अहसास होना चाहिए कि उसने किसी चीज़ का इन्तख़ाब क्यों नहीं किया। इसी सूरत में वह उन चीज़ों पर जोर दे सकता है जिसका उसने इन्तख़ाब किया है और इसी सूरत में उसे मालूम हो सकता है कि उसे अपनी मुनतसब की हुई चीज़ों पर कहाँ और कितना जोर देना चाहिए।
शायर को यह भी मालूम होना चाहिए कि उसने किसी चीज़ का इन्तख़ाब क्यों किया। उसे मालूम होना चाहिए कि उसने किसी चीज़ के बयान में किसी ख़ास सिनफ़े सुख़न और किसी ख़ास बहर का इन्तख़ाब क्यों किया है। मसनवी क्यों लिखी। मुस्द्दस में क्या बुराई थी, नज़म जिस जगह से शुरू हुई है, उसी जगह से क्यों शुरू हुई है और जहाँ ख़त्म हुई है उसी जगह ख़त्म क्यों हुई। उसे यह तमाम बातें मालूम होनी चाहिए क्योंकि जब वह तख़लीक करता है तो ख़्यालात से आँखमिचौली नहीं खेलता कि जो ख़्याल जहाँ पकड़ गया बस चोर हो गया। शायर शिकारी तो होता नहीं कि लाशऊर की तारीक झील में काँटा फेंककर बैठ जाय कि जो हाथ लग जाय। वह उससे मुतमइन नहीं होता है। शायर तो एक गृहस्थिन की तरह होता है-बाज़ार जाता है, दुकान-दुकान घूमता है, मोलतोल करता है और हर चीज़ नहीं खरीद- लेता है वहीं जीज़ें लेता है जिनकी उसे ज़रूरत होती है और जिन्हें वह ले सकता है। शायरी की बुनियाद शऊर पर होती है लाशऊर पर नहीं-वजदान शायराना लहर और इस क़िस्म की दूसरी इस्तलाहें गुमराहकुन हैं और इन्हें वही शायर इस्तेमाल करते हैं जो अपने मोहरकात से वाक़िफ नहीं होते या जो अपने मोहरकात की निशानदेही से घबराते हैं।
मरहले और भी हैं अबलापा और भी हैं।
सुन यह मुज़दा कई मैदाने वेग़ा और भी हैं।।
सुन यह मुज़दा कई मैदाने वेग़ा और भी हैं।।
लड़ाई तो उस वक़्त ख़त्म होगी जब हम जीत जायेंगे। हम न मैदान से हटें चाहे तो सदियाँ हट जाएँ।
इस बात को वाज़ा करने के लिए हिन्दुस्तानी तवारीख ने मुझे 1857 से कोई बेहतर मिसाल नहीं दी इसलिए मैंने 1857 का इन्तख़ाब किया। लेकिन 1857 इस नज़म का मौसूं नहीं है। इसका मौजूं कोई सन् नहीं है इसका मौजूं इन्सान है। जो कभी नहीं हारता। इन्सान के न हारने का यक़ीन मुझे इन्सान की तवील तवारीख ने दिलाया है। मेरे नजदीक तवारीख का मसवत काम यही है कि वह इन्सानियत पर हमारे यकीन को मोहकम करती रहती है। सुकरात जहर पी सकता है, इब्ने मरियम को मसलूब किया जा सकता है, ब्रोनो को जिन्दा जलाया जा सकता है, ऐवरेस्ट की तलाश में कई कारवाँ गुम हो सकते हैं लेकिन सुकरात हारता नहीं, ईसा की शिकस्त नहीं होती, ब्रोनो साबित क़दम रहता है और ऐवरेस्ट के गुरूर टूट जाता है।
ज़ाहिर है कि शायर इन चीज़ों की मुव्वरिख की निगाह से नहीं देखता, शायर की निगाह से देखता है इसलिए वाज औक़ात मुव्वरख़ीन इससे इख़तलाफ़ करते हैं। इस बात पर मुव्वरख़ीन में इख़तलाफे राय मुमकिन है (और है भी) कि 1857 आज़ादी की लड़ाई नहीं थी। रजवाड़ों की पेंशन की लड़ाई थी। बहादुरशाह और नानासाहब को अपनी-अपनी पेंशन की कमी का शदीद ऐहसास था। लक्ष्मीबाई दामनोदर को गद्दी पर बिठाना चाहती थी इसलिए इस तबके ने ग़ैर-मुतमइन हिन्दुस्तानी फौजियों का इस्तेमाल किया। मुझे इससे ग़रज नहीं। मैं तो इतना जानता हूँ कि यह लड़ाई अंग्रेजों के ख़िलाफ हुई। उन्नीसवीं सदी के हिन्दुस्तानी (शुमाली हिन्दुस्तानी) समाज के समान तबकों ने इस लड़ाई में शिरकत की। यही बात अहम है। मेरे लिए इस बात में कोई अहमियत नहीं रह जाती कि इन तबकों के मुक़ासित अलग-अलग थे-इन तमाम बातों को निगाह में रखने के बावजूद मैंने 1857 का इन्तख़ाब किया।
यह नज़म शायर के सफ़र से शुरू होती है। यह भी इसलिए नहीं कि नज़म को कहीं-न-कहीं से शुरू होना ही था फिर शायर के सफ़र में क्या बुराई है। जी नहीं यह नज़म शायर के इस सफंर से इसलिए शुरू होती है कि नज़म वाक़ई शायर का एक सफ़र है।
सबसे पहले मैं एक सड़क पर जाता हूँ जिसके दोरोया दरख़्तों पर लोगों की लाशें लटक रही हैं। यह सड़क मनगढ़ंत नहीं है हिन्दुस्तान में ऐसी कई सड़कें हैं। लेकिन जिस सड़क पर मैं गया वह इलाहाबाद से कानपुर की तरफ़ जाती है। यह वह तवारीखी सड़क है जिसे शेरशाह ने काफ़लों के लिए बनवाया था और जिसे अंगेजों ने लाशों के लिए इस्तेमाल किया। इस सड़क का पता मुझे अंग्रेज़ मुव्वारिख Key ने दिया था। मैंने इस सड़क का इन्तख़ाब जानबूझकर किया क्योंकि यह वह मुकाम है जहाँ से इन्क़लाब की हार भी नजर आ रही है और जीत भी। इस सड़क से जरा हटकर मुझे ज़िन्दगी की चिता में दो चिनगारियाँ मिल जाती हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि यह क्या हो रहा है। वह बता देती हैं। मैं सोचने लगता हूँ कि यह सब क्यों हो रहा है। मैं हर तबके का जायजा लेता हूँ और इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि जो हो रहा है उसे होना ही चाहिए था। मैं फिर चल पड़ता हूँ और पीछे की तरफ़ जाता हूँ। मंगल पांडे को देखता हूँ, मेरठ की लड़ाई देखता हूँ कानपुर की जंग देखता हूँ और फिर मैं लड़ाई में क़दम मिलाकर चलने लगता हूँ, इसलिए इस नज़म का ख़ातमा एक ड्रामे पर हुआ है।
जहाँ-जहाँ मैं पहुँच सका वहाँ-वहाँ पहुँच गया, मंगल पांडे की गिरफ़्तारी या मौत के वक़्त नहीं पहुँच सका तो मैंने मंगल पांडे के एक साथी को ढूँढ निकाला। उसने मुझे मंगल पांडे की कहानी सुनाई। मैं फतह देहली और शिकस्त देहली के वक़्त न पहुँच सका लेकिन रंगून के एक क़ैदखाने में चुपके से ज़रूर पहुँच गया। फिर वहाँ से मैं बहादुरशाह के साथ लालकिले में गया जहाँ वह-
इस बात को वाज़ा करने के लिए हिन्दुस्तानी तवारीख ने मुझे 1857 से कोई बेहतर मिसाल नहीं दी इसलिए मैंने 1857 का इन्तख़ाब किया। लेकिन 1857 इस नज़म का मौसूं नहीं है। इसका मौजूं कोई सन् नहीं है इसका मौजूं इन्सान है। जो कभी नहीं हारता। इन्सान के न हारने का यक़ीन मुझे इन्सान की तवील तवारीख ने दिलाया है। मेरे नजदीक तवारीख का मसवत काम यही है कि वह इन्सानियत पर हमारे यकीन को मोहकम करती रहती है। सुकरात जहर पी सकता है, इब्ने मरियम को मसलूब किया जा सकता है, ब्रोनो को जिन्दा जलाया जा सकता है, ऐवरेस्ट की तलाश में कई कारवाँ गुम हो सकते हैं लेकिन सुकरात हारता नहीं, ईसा की शिकस्त नहीं होती, ब्रोनो साबित क़दम रहता है और ऐवरेस्ट के गुरूर टूट जाता है।
ज़ाहिर है कि शायर इन चीज़ों की मुव्वरिख की निगाह से नहीं देखता, शायर की निगाह से देखता है इसलिए वाज औक़ात मुव्वरख़ीन इससे इख़तलाफ़ करते हैं। इस बात पर मुव्वरख़ीन में इख़तलाफे राय मुमकिन है (और है भी) कि 1857 आज़ादी की लड़ाई नहीं थी। रजवाड़ों की पेंशन की लड़ाई थी। बहादुरशाह और नानासाहब को अपनी-अपनी पेंशन की कमी का शदीद ऐहसास था। लक्ष्मीबाई दामनोदर को गद्दी पर बिठाना चाहती थी इसलिए इस तबके ने ग़ैर-मुतमइन हिन्दुस्तानी फौजियों का इस्तेमाल किया। मुझे इससे ग़रज नहीं। मैं तो इतना जानता हूँ कि यह लड़ाई अंग्रेजों के ख़िलाफ हुई। उन्नीसवीं सदी के हिन्दुस्तानी (शुमाली हिन्दुस्तानी) समाज के समान तबकों ने इस लड़ाई में शिरकत की। यही बात अहम है। मेरे लिए इस बात में कोई अहमियत नहीं रह जाती कि इन तबकों के मुक़ासित अलग-अलग थे-इन तमाम बातों को निगाह में रखने के बावजूद मैंने 1857 का इन्तख़ाब किया।
यह नज़म शायर के सफ़र से शुरू होती है। यह भी इसलिए नहीं कि नज़म को कहीं-न-कहीं से शुरू होना ही था फिर शायर के सफ़र में क्या बुराई है। जी नहीं यह नज़म शायर के इस सफंर से इसलिए शुरू होती है कि नज़म वाक़ई शायर का एक सफ़र है।
सबसे पहले मैं एक सड़क पर जाता हूँ जिसके दोरोया दरख़्तों पर लोगों की लाशें लटक रही हैं। यह सड़क मनगढ़ंत नहीं है हिन्दुस्तान में ऐसी कई सड़कें हैं। लेकिन जिस सड़क पर मैं गया वह इलाहाबाद से कानपुर की तरफ़ जाती है। यह वह तवारीखी सड़क है जिसे शेरशाह ने काफ़लों के लिए बनवाया था और जिसे अंगेजों ने लाशों के लिए इस्तेमाल किया। इस सड़क का पता मुझे अंग्रेज़ मुव्वारिख Key ने दिया था। मैंने इस सड़क का इन्तख़ाब जानबूझकर किया क्योंकि यह वह मुकाम है जहाँ से इन्क़लाब की हार भी नजर आ रही है और जीत भी। इस सड़क से जरा हटकर मुझे ज़िन्दगी की चिता में दो चिनगारियाँ मिल जाती हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि यह क्या हो रहा है। वह बता देती हैं। मैं सोचने लगता हूँ कि यह सब क्यों हो रहा है। मैं हर तबके का जायजा लेता हूँ और इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि जो हो रहा है उसे होना ही चाहिए था। मैं फिर चल पड़ता हूँ और पीछे की तरफ़ जाता हूँ। मंगल पांडे को देखता हूँ, मेरठ की लड़ाई देखता हूँ कानपुर की जंग देखता हूँ और फिर मैं लड़ाई में क़दम मिलाकर चलने लगता हूँ, इसलिए इस नज़म का ख़ातमा एक ड्रामे पर हुआ है।
जहाँ-जहाँ मैं पहुँच सका वहाँ-वहाँ पहुँच गया, मंगल पांडे की गिरफ़्तारी या मौत के वक़्त नहीं पहुँच सका तो मैंने मंगल पांडे के एक साथी को ढूँढ निकाला। उसने मुझे मंगल पांडे की कहानी सुनाई। मैं फतह देहली और शिकस्त देहली के वक़्त न पहुँच सका लेकिन रंगून के एक क़ैदखाने में चुपके से ज़रूर पहुँच गया। फिर वहाँ से मैं बहादुरशाह के साथ लालकिले में गया जहाँ वह-
अपने घर में
अपने वतन में
एक जानिब गरदन न्योहड़ाये
मुजरिम की मानिन्द खड़ा था
अपने वतन में
एक जानिब गरदन न्योहड़ाये
मुजरिम की मानिन्द खड़ा था
यूँ ही मैं कानपुर गया लेकिन नाना साहब की शख़्सियत मुझे देर तक न रोक सकी, वह मुझे जँचे नहीं। तो मैं गोलियों की जद से बचता अंग्रेजों के ‘किले’ में चला गया जहाँ एक हामला अंग्रेज़ औरत मौत के इस हंगामे में, शिकस्त की इस क़यामत में अपनी माजी और हाल के बारे में सोच रही थी। नाना साहब का पैगाम मेरे सामने आया। अंग्रेजों ने मेरे सामने हथियार रखे। निहत्थे अंग्रेज़ मेरे सामने गंगा की तरफ़ चले। मेरे सामने वह किश्तियों पर सवार हुए, मेरे सामने गंगा के दोनों किनारों से इन पर गोलियों की बाढ़ पड़ी।
गंगा के उजले पानी पर
क्या है कोई क्या बतलाए
जैसे कोई सुरखी ले कर
लिखता जाय मिटता जाय
क्या है कोई क्या बतलाए
जैसे कोई सुरखी ले कर
लिखता जाय मिटता जाय
यह मंजर मेरे लिए किस कदर परेशानकुन था इसका अन्दाज़ा इससे लगाइए कि इस मंजर को बयान करने में मैंने नज़मेमोअररा और नज़में आज़ाद तक के क़वानीन तक की पाबन्दी नहीं की। इतना सदीद इन्तेशार था कि शुरू के कुछ मिसरों में मैं अरकान की वहदत को भी क़ायम न रख सका। निहत्थे अंग्रेज़ों पर यह हमला उसूले जंग के मनाफी हो या न हो लेकिन मेरे नजदीक यह हमला गैर-हिन्दुस्तानी था। इसलिए नाना साहब में मेरी दिलचस्पी इतनी कम हो गई कि इनके अंजाम से मैं बेन्याज हो गया। कानपुर छोड़ने के बाद मैंने पलटकर उनकी तरफ देखने की ज़रूरत महसूस नहीं की।
मैं झाँसी की तरफ़ चल पड़ा। मुझे अपने खोये हुए एतमाद की तलाश थी। लक्ष्मीबाई के यहाँ मुझे मेरा एतमाद वापस मिला। मैंने इस बात को नज़रअन्दाज़ कर दिया कि वह क्यों लड़ रही है। मैंने तो सिर्फ़ यह देखा कि वह लड़ रही है, हिन्दुस्तानियों की तरफ लड़ रही है।
झाँसी की इस लड़ाई को भी मैं पूरी तरह न देख सका। लड़ाई का रेला कभी मुझे दूर कर देता कभी क़रीब। झाँसी वाले हिस्से में क़ुरबत और फ़ासले का यह एहसास मौजूद है। कहीं मैं इस कदर नज़दीक हूँ कि यह भी देख सकता हूँ कि दौड़ने में रानी के घोड़े का पेट पगडंडी से मिला जा रहा है और देवता भी नहीं मौजूद सनमखानों में, और कभी इतना दूर चला जाता हूँ कि तात्याँटोपे के नारों की आवाज़ तो सुन लेता हूँ लेकिन इसकी आमद और बस की शिकस्त साफ़ नजर नहीं आती।
इस भागदौड़ में मैं बहुत थक गया इसलिए जब लखनऊ पहुँचा तो मेरे लिए एक क़दम बढ़ाना भी दुश्वार हो रहा था। मैंने बूढ़े से कहा:
मैं झाँसी की तरफ़ चल पड़ा। मुझे अपने खोये हुए एतमाद की तलाश थी। लक्ष्मीबाई के यहाँ मुझे मेरा एतमाद वापस मिला। मैंने इस बात को नज़रअन्दाज़ कर दिया कि वह क्यों लड़ रही है। मैंने तो सिर्फ़ यह देखा कि वह लड़ रही है, हिन्दुस्तानियों की तरफ लड़ रही है।
झाँसी की इस लड़ाई को भी मैं पूरी तरह न देख सका। लड़ाई का रेला कभी मुझे दूर कर देता कभी क़रीब। झाँसी वाले हिस्से में क़ुरबत और फ़ासले का यह एहसास मौजूद है। कहीं मैं इस कदर नज़दीक हूँ कि यह भी देख सकता हूँ कि दौड़ने में रानी के घोड़े का पेट पगडंडी से मिला जा रहा है और देवता भी नहीं मौजूद सनमखानों में, और कभी इतना दूर चला जाता हूँ कि तात्याँटोपे के नारों की आवाज़ तो सुन लेता हूँ लेकिन इसकी आमद और बस की शिकस्त साफ़ नजर नहीं आती।
इस भागदौड़ में मैं बहुत थक गया इसलिए जब लखनऊ पहुँचा तो मेरे लिए एक क़दम बढ़ाना भी दुश्वार हो रहा था। मैंने बूढ़े से कहा:
राही अब थक के चूर है बाबा
लखनऊ कितनी दूर है बाबा
लखनऊ कितनी दूर है बाबा
मैंने लखनऊ में गोमती को समसलूब होते देखा। मैंने हज़रत महल को लखनऊ से जाते देखा, मैंने मौलवी को लखनऊ में आते देखा-और फिर मेरी जबान काट दी गई।
मैंने यह नज़्म चन्द किताबों की मदद से अपने कमरे में बैठकर नहीं लिखी है। मैंने इस लड़ाई की शिरकत की है, मैंने जख़म लगाये हैं, मैं दरख्त पर लटकाया गया हूँ, मुझे मुर्दा समझकर गिद्धों ने नोचा है। मैंने उस बेबसी को महसूस किया है जब आदमी गिद्धों से और गीदड़ों से बचने के लिए अपना जिस्म नहीं हिला सकता और जब आँखों से एक बेपनाह ख़ौफ़ बेपनाह बेबसी झलकने लगती है। मैंने उस ख़ौफ़ को भी महसूस किया है जिसे तोपदम होने से पहले हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने किया होगा। मैंने उस दीवानगी के दिन गुजारे हैं जिसमें चन्द हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने किसी मकान में किलाबन्द होकर अंग्रेजों के लश्कर को रोकने का हौसला किया था।
मैंने यह नज़्म चन्द किताबों की मदद से अपने कमरे में बैठकर नहीं लिखी है। मैंने इस लड़ाई की शिरकत की है, मैंने जख़म लगाये हैं, मैं दरख्त पर लटकाया गया हूँ, मुझे मुर्दा समझकर गिद्धों ने नोचा है। मैंने उस बेबसी को महसूस किया है जब आदमी गिद्धों से और गीदड़ों से बचने के लिए अपना जिस्म नहीं हिला सकता और जब आँखों से एक बेपनाह ख़ौफ़ बेपनाह बेबसी झलकने लगती है। मैंने उस ख़ौफ़ को भी महसूस किया है जिसे तोपदम होने से पहले हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने किया होगा। मैंने उस दीवानगी के दिन गुजारे हैं जिसमें चन्द हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने किसी मकान में किलाबन्द होकर अंग्रेजों के लश्कर को रोकने का हौसला किया था।
राही मासूम रज़ा
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book