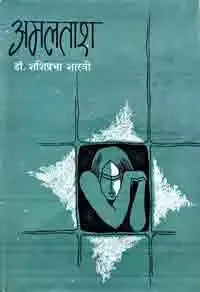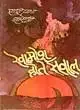|
नारी विमर्श >> अमलताश अमलताशशशिप्रभा शास्त्री
|
282 पाठक हैं |
||||||
इसमें नारी की पीड़ा की कहानी, उसके उत्सर्ग और संघर्ष की कहानी का वर्णन है
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
शशिप्रभा शास्त्री का प्रस्तुत उपन्यास एक प्रतीकात्मक उपन्यास है, जहाँ
मीदिपुर को एक रियासत बनाकर रियासतों के विलय के साथ सम्बद्ध किया गया
है-इस उपन्यास का बेशिष्टय यह है कि मीदिपुर के विलय और ध्वस्त होने के
साथ-साथ कामदा के माध्यम से नारी मात्र की भावनाओं-सम्वेदनाओं, उसके अरमान
और लालसाओं का प्रतिबिम्बन और उनका विलयन भी साथ-साथ खचित किया गया है। कामदा उपन्यास की नायिका जहाँ एक सामान्य नारी के सदृश विभिन्न कामनाओं को सँजोये चलती है, वहाँ समय आने पर एक विशिष्ट नारी की भूमिका का निर्वाह भी
उसने बड़ी निपुणता से किया है।
मानवीय संवेदनाओं को मनोविज्ञान की तुला में तौलते चलने की लेखिका की निजी शैली ने इस उपन्यास को एक नया सौष्ठव और गरिमा प्रदान की है जो प्रामाणिक होते हुए भी काल्पनिक है और काल्पनिक होते हुए भी प्रामाणिक।
कामदा जिस वास्तविकता को इस उपन्यास में ओढ़े चली है उसका अवलोकन प्रेरणाप्रद भी है और रोचक तथा रोमांचक भी। इस उपन्यास के प्राकृतिक सौन्दर्य ने अमलताश के वैभव को उजागर किया है, तो उपन्यास के समूचे वर्णन ने पुरुष की जिन्दगी के रोजनामचे को भी भरपूर खोला है
व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों प्रकार के पुस्कालयों के मूल्य की अभिवृद्धि हेतु उपन्यास की महत्ता अनिर्वचनीय।
मानवीय संवेदनाओं को मनोविज्ञान की तुला में तौलते चलने की लेखिका की निजी शैली ने इस उपन्यास को एक नया सौष्ठव और गरिमा प्रदान की है जो प्रामाणिक होते हुए भी काल्पनिक है और काल्पनिक होते हुए भी प्रामाणिक।
कामदा जिस वास्तविकता को इस उपन्यास में ओढ़े चली है उसका अवलोकन प्रेरणाप्रद भी है और रोचक तथा रोमांचक भी। इस उपन्यास के प्राकृतिक सौन्दर्य ने अमलताश के वैभव को उजागर किया है, तो उपन्यास के समूचे वर्णन ने पुरुष की जिन्दगी के रोजनामचे को भी भरपूर खोला है
व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों प्रकार के पुस्कालयों के मूल्य की अभिवृद्धि हेतु उपन्यास की महत्ता अनिर्वचनीय।
दो शब्द
भरी गर्मी में अमलताश फूलता है। जब संपूर्ण वनस्पति संसार कुम्हलाया हुआ
होता है, तो इसका आँचल रेशमी बसंती फूलों से भरा रहता है, मरे हुए मनों को
जिलाने के लिए अमलताश जीता है। पर कामदा के लिए अमलताश अभिशाप बन गया।
उसकी छाया में कामदा की कामनाएँ फूल-फूल कर जलती-झुलसती रहीं।
कामदा-स्वतंत्रता पूर्व के रजवाड़ों के सुख-वैभव के कठघरे में बँधी एक
त्रस्त-ध्वस्त ललना-जिसकी दर्द-भरी कहानी को लेकर यह
‘अमलताश’
फला फूला है, इसकी टहनियों में कामदा की भावनाएँ एक सामान्य नारी की
भावनाओं की तरह उलझी लिपटी चली हैं। अमलताल के ही माध्यम से उस काल की एक
नारी की पीड़ा को पिरोने का प्रयत्न इस कहानी में किया गया है।
स्वतंत्रता के सूर्य के उदय होने पर राजे-रजवाड़े सब लुप्त हो चुके हैं, पर नारी की पीड़ा की कहानी, उसके उत्सर्ग और संघर्ष की कहानी किसी भी युग में मिट सकेगी, इसमें संदेह है।
स्वतंत्रता के सूर्य के उदय होने पर राजे-रजवाड़े सब लुप्त हो चुके हैं, पर नारी की पीड़ा की कहानी, उसके उत्सर्ग और संघर्ष की कहानी किसी भी युग में मिट सकेगी, इसमें संदेह है।
-लेखिका
एक
सामने खड़े पेड़ों के गहरे हरे पत्तों के झुरमुट से झाँकती सबेरे की कच्ची
धूप धरती की घास पर उगे नन्हे-नन्हे प्याजी और कासनी फूलों को चूम रही थी।
कामदा ने एक हलकी अँगड़ाई लेकर झिझरियों से देखा। पवन का एक झोंका कामदा
की असलाई लटों को बिखेर गया। हृदय में नन्हा सा उल्लास जगा, नए घर की नई
सिहरन, नई गुदगुदी। तभी दासी ने आकर आदाब बजाया-
‘हुजूर, गुसल तैयार है।’
‘अच्छा। बड़ी सरकार स्नान कर चुकीं ?’
‘जी हाँ। स्नान करके वो तो अपने पूजाघर में भी पहुँच चुकी हैं।
अब आप ही रही हैं, बस। बड़ी सरकार ने ही कहलवाया है।’
‘अच्छा चलती हूँ।’ कामदा उठकर खड़ी हो गई। पीछे-पीछे दासी, आगे आगे कामदा। कामदा को स्नानागार तक पहुँचाकर दासी मुड़ गई। स्नानागार में कामदा के कीमती वस्त्र चंदन की खूँटियों पर टँगे थे। स्नान की सभी आवश्यक चीजें यथास्थान रखी थीं। पानी में से गुलाब की भीनी भीनी सुगंध फूट रही थी। कामदा की निर्वस्त्र देह इधर उधर दीवारों पर जड़े अनगिनत शीशों में नाच उठी। कामदा इधर-उधर बिखरे अपने रूप को आँखों से बेसुध होकर पीने लगी-ओठों की गुलाब सरीखी पंखुरियों के नीचे उद्दंड खड़े संगमरमरी उरोज। दृष्टि अपने आप लजा गई, गालों पर अनजाने ही केसरी आभा छाने लगी। आज तो आएँगे वे। एक हल्की सी गुदगुदी हृदय में फिर जगी और कामदा मदमस्त हुई देर तक पानी के सफेद टब में डूबी रही। स्नान करके बाहर निकली तो मोती की तरह उजली, धूप-सी पवित्र उसकी देह, रेशम की तरह चमकीली प्रतीत हो रही थी।
‘आज छोटे हुजूर हवेली में आएँगे न ?’ कामदा ने बाल सँवारती हुई दासी से पूछा।
‘जी, सरकार आज आएँगे।’ दासी ने घने सुंदर बालों को पीठ पर बिखरा दिया था। बालों की सुनहरी चमक वासंती धूप-सी नशीली प्रतीत हो रही थी।
‘आज बाल बहुत अच्छी तरह गूँथना है, ! हाँ, पर तेरा नाम क्या है, नाम तो बता अपना।’ बालों को लपेट लपेटकर छल्ले बनाते हुए कामदा के पौरुए क्षण-भर को यों ही ठिठके खड़े रहे।
‘मेरा नाम हुजूर, मेरा नाम जूही है।’ पीठ पीछे बाल सँवारती जूही नाम की दासी के अधरों पर मुसकान की नन्ही-सी लचक कामदा ने सामने खड़े दर्पण में देखी।
कामदा ने फिर कहा, ‘‘जूही तो फूल का नाम है न। पर खैर, है बहुत प्यारा। तू भी तो प्यारी सी है न, तभी तेरे माँ बाप ने तेरा नाम जूही रख दिया होगा।’ कामदा ने बालों को कंधे से आगे वक्ष पर सहलाते हुए कहा-
‘कहीं भी तो नहीं सरकार, आप बेकार-।’ और जूही लजा गई। कामदा को जूही का लजाना बहुत प्यारा लगा, पर वह इस बार कुछ बोली नहीं। जूही ने ही बताया, ‘सरकार, सुनते हैं मेरी माँ को जूही का फूल बहुत भाता था। बाप से कहा करती थीं, अगर मेरे लड़की हुई तो उसका नाम मैं जूही रखूँगी, बस इसीलिए-।’
‘हुँ।’ कामदा ने हुंकारा भरा। उसकी आँखें अपने बालों के कुंडलों को फिर निहारने लगीं, ‘तुझे भी तो जूही का फूल अच्छा लगता होगा ?’
‘जी सरकार !’ जूही का स्वर इस बार बहुत धीमा था।
‘सुन, जूही के फूल में ही मत उलझी रह जाना, आज मेरे बाल तुझे अच्छी तरह सँभालने हैं न-!’ कामदा ने याद दिलाई।
‘जी सरकार।’ और जूही के हाथ की कंघी बड़ी कोमलता से कामदा के बालों में फिर तैरने लगी। सुगंध से सारा कक्ष नहा उठा।
टोकरा-भर घने बालों का जूड़ा गूँथ जूही ने उसे फूलों की वेणी से ढाँप दिया। कोनों के कर्णफूल साड़ी से मिलते रंग के बदल दिए। कंठ के आभूषणों का डिब्बा बड़े अदब से कामदा के सामने रखते हुए उसने कहा-
‘हुजूर, अपने आप देख लें जो चाहें। कामदा चुपचाप अनेक प्रकार की मालाओं को उलट पटल करने लगी। एक बड़े बड़े सच्चे मोतियों का हार, जिसमें बीच-बीच में मानिक गुँथे थे, जिसकी हर कड़ी के साथ एक पन्ने की लड़ थी, चुनकर कामदा ने गले में डाल लिया। फिर शीशे में झाँकते हुए बोली-
‘जब तक छोटे सरकार आएँगे मैं अपने कमरे में आराम करूँगी।’
‘जी हुजूर।’ बड़े अदब से जूही कामदा को उसके कमरे में छोड़ आई। दूध से उजले गुदगुदे नरम बिस्तर पर कामदा झुक गई। हर साँस फूलों की महक से नहा उठी। सामने दीवारों पर बड़ी बड़ी तसवीरें लगी थीं-प्राकृतिक दृश्यों की तसवीरें-खिलता गुलाब, डूबता सूरज, ठिठका खड़ा समुद्र, उड़ते पंछी, बड़े-बड़े उद्यान-कामदा की दृष्टि धीमे-धीमे एक के बाद एक चित्र पर फिसलती चली। खुली आँखें सामने खुली खिड़की के बीच से तने खड़े सरू के पेड़ों की फुनगियों को छूने लगीं।
चार साल पहले जब वह इस हवेली में ब्याह कर आई थी तो इस कोठीनुमा हवेली का चप्पा-चप्पा बिजली के लट्टुओं से मढ़ा हुआ था-इसकी एक-एक झाड़ी एक-एक पेड़, एक-एक क्यारी और एक-एक मेहराब। चौदह बरस की गुड़िया-सी बहू उस दिन स्त्रियों के हुजूम में खो गई थी, कुर्सी मेजों की कतारें, सैकड़ों हजारों चमकीले बर्तन, आने जाने वालों की रेलपेल, चारों ओर खनखनाती हँसी, चहचहाते स्वर, खिलखिलाते चेहरे–कामदा उस दिन बस इतना-भर ही तो देख पाई थी। दो दिन इसी राग-रंग में डूबी वह फिर अपने पिता की हवेली में लौट आई थी। उसे लगा था, जैसे वह कोई बड़ा रंगीन मेला देखकर लौटी हो-पूरे चार बरस उसने माँ के आँगन में ही खाते-खेलते फिर बिता दिये थे और आज वह फिर अपने पिया की नगरी में लौटी है। आज तो पता ही नहीं लग रहा, इतने लंबे चार बरस कैसे कहाँ पंख लगाकर उड़ गए। पूरे चार बरस उसे यही लगता रहा, कि वह एक बड़ा मीठा सपना देख चुकी है। पिया के नगर की रंगीनी उसकी आँखों में कल तक बराबर घुली हुई थी, पर आज इस पलंग पर लेटते ही न जाने कितने सूनेपन ने उसे चारों ओर से आकर जकड़ लिया है। उस रात की कनातें और शामियाने हटकर वीरानी के इतने सारे चंदोबे कामदा के हृदय पर जाने कहां से टँग गए।
कामदा की आँखें झँपने लगीं। हवेली के विराट सूनेपन से हटकर वह कल छोड़े हुए कोलाहल में खोने लगी-माँ की प्रतिमा सामने आकर खड़ी हो गई-‘बेटी, दोनों कुल उजागर करना लाड़ो।’ पिता भीगी आँखों से अपनी गुलाब-सी बेटी के सिर पर हाथ फेर रहे थे। छोटी बहन शारदा बहन के हाथ की मुट्ठी थामे सुबक कर रो उठी थी। कामदा चार घोड़ों वाली बग्घी में बैठी तो घर के सामने नौकर-चाकरों की कतार की कतार खड़ी थी। आँखें गीली, बोल, भारी। और कामदा सबसे छुटकर अमलतास वाली कोठी के दीवान की पुत्र-वधू बनकर आ गई थी। बहू की बग्घी पर रुपये लुटा दिये थे ससुर ने। बहू का द्विरागमन ही तो बेटे का असली विवाह होता है।
सोचते-सोचते कामदा की आँखे झँप गईं। आँख खुली तो सामने जूही खड़ी थी, वह सुबह वाली दासी।
‘हुजूर, खाना तैयार है। उधर चलेंगी या इधर ही रहेंगी ?’
कामदा ने आँखें मसलकर देखा-‘जूही तू ?’
‘जी सरकार।’
‘क्या वक्त है ?’
‘हुजूर, एक-सवा बजा होगा।’
‘छोटे सरकार आ गए ? बाहर से वापस लौटे ?’ बड़ी ललक थी कामदा के स्वर में।
‘जी अभी तो नहीं ! बड़ी सरकार ने कहलाया है, आप देर न करें, किसी का इंतजार न करें, खाना खा लें।’
‘बड़ी सरकार ने कहलाया है ?’ कामदा काँप उठी। बड़ी सरकार का स्वर हल्का है, पर उसकी गूँज दूर तक सुनाई देती है। कामदा ने धीमे से कहा-
‘आती हूँ, जरा मुँह धोऊँगी।’ कामदा उठकर खड़ी हो गई। दासी दौड़कर चाँदी के लोटे में पानी ले आई। हाथ धोकर कामदा पच्चीकारी से मढ़े हुए बरामदे में धीमे-धीमे कदम रखती हुई खाने के कक्ष में आकर खड़ी हो गई।
‘बहूरानी, कल रात भी तुमने कुछ नहीं खाया। खाना खा लो।’ कामदा बिना किसी ना नुच के चाँदी से मढ़ी चंदन की चौकी के सामने बैठ गई। सास पास बैठीं। दासी को आदेश दिया गया-
‘खाना लाओ।’
एक बड़ा-सा चाँदी का थाल सजकर मेज पर आ गया। अनगिनत कटोरियाँ-सब्जी, चटनी, खीर और रायते से भरी हुई।
‘खाओ बहूरानी।’ एक दूसरा आदेश पास से उठा।
‘आप ?’ कामदा ने छोटी-सी नजर उठाई।
‘मैं तुम्हारे ससुर, दीवान साहब के आने पर बाद में खाऊँगी, यों भी आज पूर्णिमा है, जल्दी खाने का सवाल नहीं उठता,’ सास ने स्पष्ट स्वर में समझाया।
‘तो मैं कैसे-सबसे पहले-’ आगे के शब्द बीच में ही रह गए। टाइलों के फर्श वाले आँगन में तेज धूप बिखरी हुई थी और छत की मुंडेर पर बैठे काग की परछाईं आँगन के बीचों-बीच एक तसवीर सी लग रही थी।
‘तुम खा लो। तुम अभी बच्चा हो । इतनी भूख नहीं सहार पाओगी, खाओ !’ फिर आदेश का दूसरा कोड़ा कामदा के कानों पर सड़ाक से बजा।
कामदा ने खाना शुरू किया, एक ग्रास दो ग्रास तीन ग्रास। फिर हाथ रुक गया, ओठ बंद हो गए, जबान तालू से सट गई।
‘क्या बात है बहू ? रुक क्यों गईं ? खा क्यों नहीं रहीं ?’
‘भूख नहीं है माँ।’ कामदा ने कहा तो बड़ी सरकार ने दासी को आवाज दी-
‘देविका।’
‘जी।’
‘थाल उठाकर ले जाओ।’
पूरा थाल ज्यों का त्यों उठकर चला गया। कामदा यों ही चुपचाप बैठी रही।
‘हाथ धो डालो।’
‘जी।’ कामदा उठी, सामने खड़ी दासी ने चिलमची आगे कर दी। पान का बीड़ा चाँदी की तश्तरी में लगकर पीछे-पीछे आ गया। कामदा ने पान मुँह में रखा, फिर खिड़की के बाहर थूक दिया और चुपचाप पलंग पर लेट गई।
सड़क पर घोड़ागाड़ी फिसल रही थी। घोड़ों की टापों का स्वर, उनके गले में लटकती घंटियों की झनन झनन कामदा के कानों में पड़ी। वह उठकर बैठी नहीं, चुपचाप लेटी रही। उसके कान सुनते रहे, आँखें सामने दीवार पर देखती रहीं-दीवान साहब, बड़ी-बड़ी तनी हुई मूँछें, छोटी-छोटी पर पैनी आँखें, नुकीली नाक बड़ी सी दाढ़ी गले में मोतियों का कंठा, कामदार शेरवानी सलीमशाही जूतियाँ ऊँचा-लंबा कद अमलतास के पेड़ों की छाया को लाँघते लाल बजरी वाली सड़क पर चलते हुए बारादरी, बरामदे दर बरामदे पार करते हुए बिलकुल भीतर आ खड़े हुए। बड़ी सरकार पति की रौबीली चितवन से हड़बड़ाकर उठीं। दास-दासियाँ भाग चले और आदेश की प्रतीक्षा में घेरा बाँधकर खड़े हो गए, उनके अंतरंग कक्ष में पहुँचने पर एक सलीमशाही जूतियाँ हल्के से पैरों से उतारकर सादी मखमली जूतियाँ अटका दीं। दूसरे ने हल्के से अचकन उतारी, पटका थामा और फिर खाने के कक्ष में भगदड़ मच गई-
‘‘बहू ने खाना खा लिया ?’
‘जी खा भी लिया, नहीं भी खाया। बहू सबसे पहले खाना नहीं खाना चाहतीं। फिर आप इतनी देर में आते हैं, बच्ची ही तो है, कब तक भूखी रखूँ।’
‘हु। बहू के पास फल-वल भिजवा दो, कल से हम जल्द आने की कोशिश करेंगे।’
दासी ने सब कुछ कामदा को जाकर सुनाया तो कामदा की आँखों में आँसू छलछला आए। उसके ससुर कितनी मुलायम तबियत के हैं ! कामदा को आश्चर्य हुआ कैसा घर है यह जिसके कुँवर के कभी दर्शन ही नहीं होते।
दिन ढल गया। घोड़ागाड़ी झनन झनन करती हुई मीदिपुर के दीवान साहब को फिर अहाते से बाहर ले गई। कामदा ने खिड़की से झाँककर देखा, शाम के साये गहरे होते चले जा रहे थे। कमरे में लगी चमकीली तस्वीरें धुँधली पड़ने लगीं।
दासी ने आकर कमरे में फानूस जला दिया, ‘अंधकार चमचमा उठा।
‘अभी तक मेरे छोटे सरकार नहीं आए, जूही ?’ कामदा की ओर से एक फुसफुसाता स्वर उठा।
‘नहीं सरकार, अभी बड़ी सरकार साहिबा आएँगी, उनसे पूछ लें।’
‘बड़ी सरकार यहाँ आएँगी, मेरे कमरे में ?’
‘जी।’ कहकर जूही बाहर चली गई। चेहरे पर एक विशेष प्रकार का पियाला छा गया।
कामदा बड़ी सरकार की प्रतीक्षा करने लगी। हर पल उसकी देह काँप उठती थी। वह कल भी अकेली सोई थी। बड़ी सरकार ने कल शाम खाना कमरे में ही भिजवा दिया था, पर कामदा को कल भी कुछ नहीं रुचा था। अच्छा है, बड़ी सरकार खाने के समय आज खुद आएँगी तब वह यह सब कुछ खुद पूछेगी ! इस घर के छोटे सरकार कहाँ रहते हैं, क्या-क्या करते हैं, घर में क्यों नहीं आते ?
ये सब बातें वह जूही से भी तो पूछ सकती है, पर जूही नौकरानी है, क्या पता किसी से क्या कहे। नहीं, जूही से वह कुछ नहीं पूछेगी, आज तो माँ से ही सब कुछ पूछ लूँगी। ठीक है। मन ने हामी भरी पर शाम को केवल भोजन का थाल फिर आ पहुँचा। बड़ी सरकार नहीं आई। जूही से उन्होंने कहलवा दिया-
‘हरदेवलाल पढ़ाई के लिए बाहर रहते हैं। पढ़ाई खतम करके ही लौटेंगे। इतने लंबे समय तक कोई भूखा नहीं रह सकता।’
‘हुजूर, गुसल तैयार है।’
‘अच्छा। बड़ी सरकार स्नान कर चुकीं ?’
‘जी हाँ। स्नान करके वो तो अपने पूजाघर में भी पहुँच चुकी हैं।
अब आप ही रही हैं, बस। बड़ी सरकार ने ही कहलवाया है।’
‘अच्छा चलती हूँ।’ कामदा उठकर खड़ी हो गई। पीछे-पीछे दासी, आगे आगे कामदा। कामदा को स्नानागार तक पहुँचाकर दासी मुड़ गई। स्नानागार में कामदा के कीमती वस्त्र चंदन की खूँटियों पर टँगे थे। स्नान की सभी आवश्यक चीजें यथास्थान रखी थीं। पानी में से गुलाब की भीनी भीनी सुगंध फूट रही थी। कामदा की निर्वस्त्र देह इधर उधर दीवारों पर जड़े अनगिनत शीशों में नाच उठी। कामदा इधर-उधर बिखरे अपने रूप को आँखों से बेसुध होकर पीने लगी-ओठों की गुलाब सरीखी पंखुरियों के नीचे उद्दंड खड़े संगमरमरी उरोज। दृष्टि अपने आप लजा गई, गालों पर अनजाने ही केसरी आभा छाने लगी। आज तो आएँगे वे। एक हल्की सी गुदगुदी हृदय में फिर जगी और कामदा मदमस्त हुई देर तक पानी के सफेद टब में डूबी रही। स्नान करके बाहर निकली तो मोती की तरह उजली, धूप-सी पवित्र उसकी देह, रेशम की तरह चमकीली प्रतीत हो रही थी।
‘आज छोटे हुजूर हवेली में आएँगे न ?’ कामदा ने बाल सँवारती हुई दासी से पूछा।
‘जी, सरकार आज आएँगे।’ दासी ने घने सुंदर बालों को पीठ पर बिखरा दिया था। बालों की सुनहरी चमक वासंती धूप-सी नशीली प्रतीत हो रही थी।
‘आज बाल बहुत अच्छी तरह गूँथना है, ! हाँ, पर तेरा नाम क्या है, नाम तो बता अपना।’ बालों को लपेट लपेटकर छल्ले बनाते हुए कामदा के पौरुए क्षण-भर को यों ही ठिठके खड़े रहे।
‘मेरा नाम हुजूर, मेरा नाम जूही है।’ पीठ पीछे बाल सँवारती जूही नाम की दासी के अधरों पर मुसकान की नन्ही-सी लचक कामदा ने सामने खड़े दर्पण में देखी।
कामदा ने फिर कहा, ‘‘जूही तो फूल का नाम है न। पर खैर, है बहुत प्यारा। तू भी तो प्यारी सी है न, तभी तेरे माँ बाप ने तेरा नाम जूही रख दिया होगा।’ कामदा ने बालों को कंधे से आगे वक्ष पर सहलाते हुए कहा-
‘कहीं भी तो नहीं सरकार, आप बेकार-।’ और जूही लजा गई। कामदा को जूही का लजाना बहुत प्यारा लगा, पर वह इस बार कुछ बोली नहीं। जूही ने ही बताया, ‘सरकार, सुनते हैं मेरी माँ को जूही का फूल बहुत भाता था। बाप से कहा करती थीं, अगर मेरे लड़की हुई तो उसका नाम मैं जूही रखूँगी, बस इसीलिए-।’
‘हुँ।’ कामदा ने हुंकारा भरा। उसकी आँखें अपने बालों के कुंडलों को फिर निहारने लगीं, ‘तुझे भी तो जूही का फूल अच्छा लगता होगा ?’
‘जी सरकार !’ जूही का स्वर इस बार बहुत धीमा था।
‘सुन, जूही के फूल में ही मत उलझी रह जाना, आज मेरे बाल तुझे अच्छी तरह सँभालने हैं न-!’ कामदा ने याद दिलाई।
‘जी सरकार।’ और जूही के हाथ की कंघी बड़ी कोमलता से कामदा के बालों में फिर तैरने लगी। सुगंध से सारा कक्ष नहा उठा।
टोकरा-भर घने बालों का जूड़ा गूँथ जूही ने उसे फूलों की वेणी से ढाँप दिया। कोनों के कर्णफूल साड़ी से मिलते रंग के बदल दिए। कंठ के आभूषणों का डिब्बा बड़े अदब से कामदा के सामने रखते हुए उसने कहा-
‘हुजूर, अपने आप देख लें जो चाहें। कामदा चुपचाप अनेक प्रकार की मालाओं को उलट पटल करने लगी। एक बड़े बड़े सच्चे मोतियों का हार, जिसमें बीच-बीच में मानिक गुँथे थे, जिसकी हर कड़ी के साथ एक पन्ने की लड़ थी, चुनकर कामदा ने गले में डाल लिया। फिर शीशे में झाँकते हुए बोली-
‘जब तक छोटे सरकार आएँगे मैं अपने कमरे में आराम करूँगी।’
‘जी हुजूर।’ बड़े अदब से जूही कामदा को उसके कमरे में छोड़ आई। दूध से उजले गुदगुदे नरम बिस्तर पर कामदा झुक गई। हर साँस फूलों की महक से नहा उठी। सामने दीवारों पर बड़ी बड़ी तसवीरें लगी थीं-प्राकृतिक दृश्यों की तसवीरें-खिलता गुलाब, डूबता सूरज, ठिठका खड़ा समुद्र, उड़ते पंछी, बड़े-बड़े उद्यान-कामदा की दृष्टि धीमे-धीमे एक के बाद एक चित्र पर फिसलती चली। खुली आँखें सामने खुली खिड़की के बीच से तने खड़े सरू के पेड़ों की फुनगियों को छूने लगीं।
चार साल पहले जब वह इस हवेली में ब्याह कर आई थी तो इस कोठीनुमा हवेली का चप्पा-चप्पा बिजली के लट्टुओं से मढ़ा हुआ था-इसकी एक-एक झाड़ी एक-एक पेड़, एक-एक क्यारी और एक-एक मेहराब। चौदह बरस की गुड़िया-सी बहू उस दिन स्त्रियों के हुजूम में खो गई थी, कुर्सी मेजों की कतारें, सैकड़ों हजारों चमकीले बर्तन, आने जाने वालों की रेलपेल, चारों ओर खनखनाती हँसी, चहचहाते स्वर, खिलखिलाते चेहरे–कामदा उस दिन बस इतना-भर ही तो देख पाई थी। दो दिन इसी राग-रंग में डूबी वह फिर अपने पिता की हवेली में लौट आई थी। उसे लगा था, जैसे वह कोई बड़ा रंगीन मेला देखकर लौटी हो-पूरे चार बरस उसने माँ के आँगन में ही खाते-खेलते फिर बिता दिये थे और आज वह फिर अपने पिया की नगरी में लौटी है। आज तो पता ही नहीं लग रहा, इतने लंबे चार बरस कैसे कहाँ पंख लगाकर उड़ गए। पूरे चार बरस उसे यही लगता रहा, कि वह एक बड़ा मीठा सपना देख चुकी है। पिया के नगर की रंगीनी उसकी आँखों में कल तक बराबर घुली हुई थी, पर आज इस पलंग पर लेटते ही न जाने कितने सूनेपन ने उसे चारों ओर से आकर जकड़ लिया है। उस रात की कनातें और शामियाने हटकर वीरानी के इतने सारे चंदोबे कामदा के हृदय पर जाने कहां से टँग गए।
कामदा की आँखें झँपने लगीं। हवेली के विराट सूनेपन से हटकर वह कल छोड़े हुए कोलाहल में खोने लगी-माँ की प्रतिमा सामने आकर खड़ी हो गई-‘बेटी, दोनों कुल उजागर करना लाड़ो।’ पिता भीगी आँखों से अपनी गुलाब-सी बेटी के सिर पर हाथ फेर रहे थे। छोटी बहन शारदा बहन के हाथ की मुट्ठी थामे सुबक कर रो उठी थी। कामदा चार घोड़ों वाली बग्घी में बैठी तो घर के सामने नौकर-चाकरों की कतार की कतार खड़ी थी। आँखें गीली, बोल, भारी। और कामदा सबसे छुटकर अमलतास वाली कोठी के दीवान की पुत्र-वधू बनकर आ गई थी। बहू की बग्घी पर रुपये लुटा दिये थे ससुर ने। बहू का द्विरागमन ही तो बेटे का असली विवाह होता है।
सोचते-सोचते कामदा की आँखे झँप गईं। आँख खुली तो सामने जूही खड़ी थी, वह सुबह वाली दासी।
‘हुजूर, खाना तैयार है। उधर चलेंगी या इधर ही रहेंगी ?’
कामदा ने आँखें मसलकर देखा-‘जूही तू ?’
‘जी सरकार।’
‘क्या वक्त है ?’
‘हुजूर, एक-सवा बजा होगा।’
‘छोटे सरकार आ गए ? बाहर से वापस लौटे ?’ बड़ी ललक थी कामदा के स्वर में।
‘जी अभी तो नहीं ! बड़ी सरकार ने कहलाया है, आप देर न करें, किसी का इंतजार न करें, खाना खा लें।’
‘बड़ी सरकार ने कहलाया है ?’ कामदा काँप उठी। बड़ी सरकार का स्वर हल्का है, पर उसकी गूँज दूर तक सुनाई देती है। कामदा ने धीमे से कहा-
‘आती हूँ, जरा मुँह धोऊँगी।’ कामदा उठकर खड़ी हो गई। दासी दौड़कर चाँदी के लोटे में पानी ले आई। हाथ धोकर कामदा पच्चीकारी से मढ़े हुए बरामदे में धीमे-धीमे कदम रखती हुई खाने के कक्ष में आकर खड़ी हो गई।
‘बहूरानी, कल रात भी तुमने कुछ नहीं खाया। खाना खा लो।’ कामदा बिना किसी ना नुच के चाँदी से मढ़ी चंदन की चौकी के सामने बैठ गई। सास पास बैठीं। दासी को आदेश दिया गया-
‘खाना लाओ।’
एक बड़ा-सा चाँदी का थाल सजकर मेज पर आ गया। अनगिनत कटोरियाँ-सब्जी, चटनी, खीर और रायते से भरी हुई।
‘खाओ बहूरानी।’ एक दूसरा आदेश पास से उठा।
‘आप ?’ कामदा ने छोटी-सी नजर उठाई।
‘मैं तुम्हारे ससुर, दीवान साहब के आने पर बाद में खाऊँगी, यों भी आज पूर्णिमा है, जल्दी खाने का सवाल नहीं उठता,’ सास ने स्पष्ट स्वर में समझाया।
‘तो मैं कैसे-सबसे पहले-’ आगे के शब्द बीच में ही रह गए। टाइलों के फर्श वाले आँगन में तेज धूप बिखरी हुई थी और छत की मुंडेर पर बैठे काग की परछाईं आँगन के बीचों-बीच एक तसवीर सी लग रही थी।
‘तुम खा लो। तुम अभी बच्चा हो । इतनी भूख नहीं सहार पाओगी, खाओ !’ फिर आदेश का दूसरा कोड़ा कामदा के कानों पर सड़ाक से बजा।
कामदा ने खाना शुरू किया, एक ग्रास दो ग्रास तीन ग्रास। फिर हाथ रुक गया, ओठ बंद हो गए, जबान तालू से सट गई।
‘क्या बात है बहू ? रुक क्यों गईं ? खा क्यों नहीं रहीं ?’
‘भूख नहीं है माँ।’ कामदा ने कहा तो बड़ी सरकार ने दासी को आवाज दी-
‘देविका।’
‘जी।’
‘थाल उठाकर ले जाओ।’
पूरा थाल ज्यों का त्यों उठकर चला गया। कामदा यों ही चुपचाप बैठी रही।
‘हाथ धो डालो।’
‘जी।’ कामदा उठी, सामने खड़ी दासी ने चिलमची आगे कर दी। पान का बीड़ा चाँदी की तश्तरी में लगकर पीछे-पीछे आ गया। कामदा ने पान मुँह में रखा, फिर खिड़की के बाहर थूक दिया और चुपचाप पलंग पर लेट गई।
सड़क पर घोड़ागाड़ी फिसल रही थी। घोड़ों की टापों का स्वर, उनके गले में लटकती घंटियों की झनन झनन कामदा के कानों में पड़ी। वह उठकर बैठी नहीं, चुपचाप लेटी रही। उसके कान सुनते रहे, आँखें सामने दीवार पर देखती रहीं-दीवान साहब, बड़ी-बड़ी तनी हुई मूँछें, छोटी-छोटी पर पैनी आँखें, नुकीली नाक बड़ी सी दाढ़ी गले में मोतियों का कंठा, कामदार शेरवानी सलीमशाही जूतियाँ ऊँचा-लंबा कद अमलतास के पेड़ों की छाया को लाँघते लाल बजरी वाली सड़क पर चलते हुए बारादरी, बरामदे दर बरामदे पार करते हुए बिलकुल भीतर आ खड़े हुए। बड़ी सरकार पति की रौबीली चितवन से हड़बड़ाकर उठीं। दास-दासियाँ भाग चले और आदेश की प्रतीक्षा में घेरा बाँधकर खड़े हो गए, उनके अंतरंग कक्ष में पहुँचने पर एक सलीमशाही जूतियाँ हल्के से पैरों से उतारकर सादी मखमली जूतियाँ अटका दीं। दूसरे ने हल्के से अचकन उतारी, पटका थामा और फिर खाने के कक्ष में भगदड़ मच गई-
‘‘बहू ने खाना खा लिया ?’
‘जी खा भी लिया, नहीं भी खाया। बहू सबसे पहले खाना नहीं खाना चाहतीं। फिर आप इतनी देर में आते हैं, बच्ची ही तो है, कब तक भूखी रखूँ।’
‘हु। बहू के पास फल-वल भिजवा दो, कल से हम जल्द आने की कोशिश करेंगे।’
दासी ने सब कुछ कामदा को जाकर सुनाया तो कामदा की आँखों में आँसू छलछला आए। उसके ससुर कितनी मुलायम तबियत के हैं ! कामदा को आश्चर्य हुआ कैसा घर है यह जिसके कुँवर के कभी दर्शन ही नहीं होते।
दिन ढल गया। घोड़ागाड़ी झनन झनन करती हुई मीदिपुर के दीवान साहब को फिर अहाते से बाहर ले गई। कामदा ने खिड़की से झाँककर देखा, शाम के साये गहरे होते चले जा रहे थे। कमरे में लगी चमकीली तस्वीरें धुँधली पड़ने लगीं।
दासी ने आकर कमरे में फानूस जला दिया, ‘अंधकार चमचमा उठा।
‘अभी तक मेरे छोटे सरकार नहीं आए, जूही ?’ कामदा की ओर से एक फुसफुसाता स्वर उठा।
‘नहीं सरकार, अभी बड़ी सरकार साहिबा आएँगी, उनसे पूछ लें।’
‘बड़ी सरकार यहाँ आएँगी, मेरे कमरे में ?’
‘जी।’ कहकर जूही बाहर चली गई। चेहरे पर एक विशेष प्रकार का पियाला छा गया।
कामदा बड़ी सरकार की प्रतीक्षा करने लगी। हर पल उसकी देह काँप उठती थी। वह कल भी अकेली सोई थी। बड़ी सरकार ने कल शाम खाना कमरे में ही भिजवा दिया था, पर कामदा को कल भी कुछ नहीं रुचा था। अच्छा है, बड़ी सरकार खाने के समय आज खुद आएँगी तब वह यह सब कुछ खुद पूछेगी ! इस घर के छोटे सरकार कहाँ रहते हैं, क्या-क्या करते हैं, घर में क्यों नहीं आते ?
ये सब बातें वह जूही से भी तो पूछ सकती है, पर जूही नौकरानी है, क्या पता किसी से क्या कहे। नहीं, जूही से वह कुछ नहीं पूछेगी, आज तो माँ से ही सब कुछ पूछ लूँगी। ठीक है। मन ने हामी भरी पर शाम को केवल भोजन का थाल फिर आ पहुँचा। बड़ी सरकार नहीं आई। जूही से उन्होंने कहलवा दिया-
‘हरदेवलाल पढ़ाई के लिए बाहर रहते हैं। पढ़ाई खतम करके ही लौटेंगे। इतने लंबे समय तक कोई भूखा नहीं रह सकता।’
दो
तहसीलदार त्रिभुवनसिंह ने ड्यौढ़ी में प्रवेश करते ही पूछा-
‘कामदा की कोई चिट्ठी आई ?’
‘नहीं तो’, पत्नी रामकुँअर ने पान लगाते लगाते जवाब दिया और फिर उनकी आँखें गीली हो उठीं।
‘अरे इतना मन छोटा क्यों करती हो। कामदा अभी बच्ची है, जिम्मेदारी नहीं पहचानती। फिर अपने घर रह-बसकर लड़कियाँ माँ-बाप को उतना याद भी कहाँ रखती हैं।’ त्रिभुवनसिंह ने अचकन उतारकर खूँटी पर टाँग दी और फिर पान लगाती पत्नी के पास तख्तपर आकर बैठलगए।
‘कुछ झूठ कहा है मैंने ?’ त्रिभुवनसिंह ने पत्नी की आँखों में झाँकने का प्रयत्न किया।
‘चलो हटो, तुम क्या समझो लड़की के दिल की। लड़कियाँ अपने माँ बाप के घर-द्वार को कभी नहीं भूलतीं। फिर मेरी कामदा ऐसी है भी नहीं, उसके बराबर कच्चे दिल वाला कोई होगा। देखा नहीं था, जाते वक्त कैसी आठ-आठ आँसू रोई थी। मुझे तो यही चिंता है, लड़की वहाँ कैसे रह बस रही होगी। अभी कच्ची उमर है; सत्रह-अठारह बरस की उमर होती भी क्या है।’
‘कामदा की कोई चिट्ठी आई ?’
‘नहीं तो’, पत्नी रामकुँअर ने पान लगाते लगाते जवाब दिया और फिर उनकी आँखें गीली हो उठीं।
‘अरे इतना मन छोटा क्यों करती हो। कामदा अभी बच्ची है, जिम्मेदारी नहीं पहचानती। फिर अपने घर रह-बसकर लड़कियाँ माँ-बाप को उतना याद भी कहाँ रखती हैं।’ त्रिभुवनसिंह ने अचकन उतारकर खूँटी पर टाँग दी और फिर पान लगाती पत्नी के पास तख्तपर आकर बैठलगए।
‘कुछ झूठ कहा है मैंने ?’ त्रिभुवनसिंह ने पत्नी की आँखों में झाँकने का प्रयत्न किया।
‘चलो हटो, तुम क्या समझो लड़की के दिल की। लड़कियाँ अपने माँ बाप के घर-द्वार को कभी नहीं भूलतीं। फिर मेरी कामदा ऐसी है भी नहीं, उसके बराबर कच्चे दिल वाला कोई होगा। देखा नहीं था, जाते वक्त कैसी आठ-आठ आँसू रोई थी। मुझे तो यही चिंता है, लड़की वहाँ कैसे रह बस रही होगी। अभी कच्ची उमर है; सत्रह-अठारह बरस की उमर होती भी क्या है।’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book