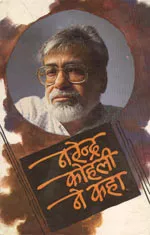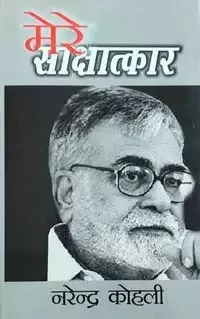|
जीवनी/आत्मकथा >> नरेन्द्र कोहली ने कहा नरेन्द्र कोहली ने कहानरेन्द्र कोहली
|
135 पाठक हैं |
||||||
इस पुस्तक के माध्यम से नरेन्द्र कोहली ने अपनी आत्मकथा का वर्णन किया है...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
कहा तो यह सब कुछ नरेन्द्र कोहली ने ही है, किन्तु इस प्रकार पुस्तक के
रूप में नहीं कहा था। कभी आत्मकथ्य के रूप में कहा, अपने विषय में बात
करते हुए, कभी अपनी सृजन प्रक्रिया में कहा और कभी किसी के प्रश्नों और
जिज्ञासाओं का उत्तर देते हुए कहा। इतना ही नहीं, लेखक की विभिन्न रचनाओं
के पात्र जो कुछ कहते हैं, वस्तुतः कहता तो वह लेखक ही है। तो यह सब
नरेन्द्र कोहली ने कहा। व्यक्ति के विषय में भी कहा और समाज के विषय में
भी। समाज के मन में भी पैठे, व्यक्ति के मन में भी और अपने मन में भी। इस
पुस्तक ने तो बस एक मंच प्रस्तुत कर दिया है, जहाँ नरेन्द्र कोहली की
उक्तियाँ मिल बैठी हैं, वक्तव्य एकत्रित हो गये हैं और अनुभव रेखांकित हो
गये हैं, यह मंच इसलिए बनाया गया, क्योंकि उसके सम्मुख बैठा श्रोता अपनी
जिज्ञासाओं का समाधान पा सके और अपने प्रश्नों की तृषा को उनके वास्तविक
उत्तरों से तृप्त कर सके।
लेखक जो कुछ अपने पात्रों के माध्यम से कहता है, जो वह अपनी बातचीत में कहता है, कहता तो अपना अनुभव ही है। तो उसके कहे से समाज और व्यक्ति मन की गुत्थियाँ तो सुलझाई ही जा सकती हैं, किन्तु उससे बड़ी बात है-एक लेखक को जानना, उसके सृजन को जानना, उसकी सृजन-प्रक्रिया को जानना, एक सर्जक साहित्यकार के अंतस को जानना, उसकी आत्मा को जानना।
हमारे पास इस प्रकार की पुस्तकें बहुत कम हैं, जिनके माध्यम से उन पुस्तकों के सृजक के वास्तविक व्यक्तित्व, उसके अंतर्मन, उसके सृजन संसार तथा उसके चिंतन को जान सकें, जो हमें बेहद प्रिय हैं। सामान्य पाठक के लिए लेखक और कलाकार जिज्ञासा की वस्तु ही बना रहता है-एक वयवीय अस्तित्व। पर यह पुस्तक आपके लिए अपने प्रिय लेखक को वायवीय अस्तित्व नहीं रहने देगी। यह उसके चिंतन को ही नहीं, उसके अनुभव को भी एक स्पष्ट रूपाकार देकर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर देगी। आप सृजन को ही नहीं, उस सर्जक को भी जान पाएँगे, जिसने वह सृजन किया है।
और फिर आप उसके चिंतन के निष्कर्षों को सूक्तियों के रूप में भी जानेंगे। इस पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात् यह कहना कठिन हो जाएगा कि हिन्दी का पाठक अपने लेखक के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, वह उससे प्रेम नहीं करता। यह पुस्तक एक पारदर्शी चिलमन है, जो आपके और लेखक के मध्य सारे पर्दे उठा देती है। आप अपने प्रिय लेखक को अपने आत्मीय के रूप में जान सकते हैं, उस तक पहुँच सकते हैं।
लेखक जो कुछ अपने पात्रों के माध्यम से कहता है, जो वह अपनी बातचीत में कहता है, कहता तो अपना अनुभव ही है। तो उसके कहे से समाज और व्यक्ति मन की गुत्थियाँ तो सुलझाई ही जा सकती हैं, किन्तु उससे बड़ी बात है-एक लेखक को जानना, उसके सृजन को जानना, उसकी सृजन-प्रक्रिया को जानना, एक सर्जक साहित्यकार के अंतस को जानना, उसकी आत्मा को जानना।
हमारे पास इस प्रकार की पुस्तकें बहुत कम हैं, जिनके माध्यम से उन पुस्तकों के सृजक के वास्तविक व्यक्तित्व, उसके अंतर्मन, उसके सृजन संसार तथा उसके चिंतन को जान सकें, जो हमें बेहद प्रिय हैं। सामान्य पाठक के लिए लेखक और कलाकार जिज्ञासा की वस्तु ही बना रहता है-एक वयवीय अस्तित्व। पर यह पुस्तक आपके लिए अपने प्रिय लेखक को वायवीय अस्तित्व नहीं रहने देगी। यह उसके चिंतन को ही नहीं, उसके अनुभव को भी एक स्पष्ट रूपाकार देकर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर देगी। आप सृजन को ही नहीं, उस सर्जक को भी जान पाएँगे, जिसने वह सृजन किया है।
और फिर आप उसके चिंतन के निष्कर्षों को सूक्तियों के रूप में भी जानेंगे। इस पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात् यह कहना कठिन हो जाएगा कि हिन्दी का पाठक अपने लेखक के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, वह उससे प्रेम नहीं करता। यह पुस्तक एक पारदर्शी चिलमन है, जो आपके और लेखक के मध्य सारे पर्दे उठा देती है। आप अपने प्रिय लेखक को अपने आत्मीय के रूप में जान सकते हैं, उस तक पहुँच सकते हैं।
बकलम खुद
मुझे बताया गया है कि मेरा जन्म 6 जनवरी, 1940 ई. को स्यालकोट में प्रातः
साढ़े नौ बजे हुआ था। जिस घर में मेरा जन्म हुआ था, वह मेरे दादा का था।
दादा पंजाब के वन-विभाग में हेड क्लर्क थे और इसी पद से रिटायर हुए थे। पर
उनकी आर्थिक स्थिति बुरी नहीं थी। होश संभालने पर जो तथ्य मुझे मालूम हुए
थे उनके आधार पर ज्ञात हुआ कि पैतृक मकान का उनका हिस्सा उनके बड़े भाई ने
हड़प लिया था। उस हिस्से को लेकर भाइयों में जो झगड़ा हुआ था वह उनके जीवन
के अन्त तक चला। मेरे दादा के देहांत पर भी उनके बड़े भाई नहीं आये थे।
पर मेरे दादा ने अपनी वैध-अवैध कमाई के आधार पर दो मकान बनवाये थे। एक मकान ‘ट्रंकां वाले बाजार’ के ‘मुहल्ला डिप्टी का बाग’ में था-जो पुराने किस्म का मकान था और किराये पर चढ़ा हुआ था। दूसरा मकान ‘मुहल्ला वाटर वर्क्स में एबट रोड पर था। यह नये क्षेत्र में खुला हवादार मकान था। दूसरा मकान था। इसमें मेरे दादा स्वयं रहते थे। उनकी दो पत्नियाँ थीं। दादा की बड़ी पत्नी-हमारी सगी दादी-अपने पति से अलग, चाचाजी के पास जमशेदपुर में रहतीं थीं। दादा अपनी दूसरी पत्नी से साथ अपने इस मकान में रहते थे। मेरे दादा का नाम हरकिशनदास और दादी का नाम भाइयां देई था। छोटी-दादी मेरी सौतेली दादी-का नाम दुर्गादेवी था। दादा उर्दू और अंग्रेजी जानते थे। शायद मैट्रिक पास थे। दादियाँ दोनों ही निरक्षर थीं।
मेरे पिता-परमानन्द कोहली-की आँखों में बचपन से कुकरे थे। दृष्टि दोषपूर्ण होने के कारण वे सातवीं-आठवीं से आगे नहीं पढ़ सके थे। दादा ने उन्हें स्यालकोट में पुस्तकों और पत्रिकाओं की एक दुकान खोल दी थी। किंतु वे दुकानदार नहीं, साहित्यकार बनना चाहते थे। उन्होंने दो एक कहानियां भी लिखी थीं, जो किसी दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित हुई थी; किंतु न वे साहित्यकार बन सके और न दुकानदार। अंग्रेजों के विरुद्ध किये गये किसी प्रदर्शन में पकड़े गये। दादा जमानत पर न केवल उन्हें छुड़ा लाये, वरन् अपने अंग्रेज अधिकारी से कहकर उन्हें अपने ही विभाग में अस्थायी क्लर्क की नौकरी दिलवा दी। समुचित रूप से शिक्षित न होने और अपने दृष्टिकोण के कारण, उनकी नौकरी न कभी पक्की हो सकी, न उनकी पदोन्नति हुई; दूसरी ओर अपने परिश्रम और अंग्रेज अधिकारी की कृपा के कारण वे नौकरी से निकाले भी नहीं जा सके। जहाँ थे, त्रिशंकु के समान वहीं टंगे रहे।
मेरी माँ-विद्यावंती-स्यालकोट के पास के ही एक गाँव ‘कौलोकी’ के कृषक परिवार से थीं। ‘कौलोकी’ में न स्कूल था, न डाकघर, न अस्पताल, न ही कुछ और। माँ सर्वथा निरक्षर थीं।
मेरा शैशव कभी भी नटखट और खिलंडरे बच्चों का शैशव नहीं रहा। आरम्भ में कदाचित मैं काफी बीमार और रोना बच्चा रहा होऊँगा। शरीर पर फोड़े-फुंसियाँ भी बहुत थीं। अधिकांशतः माँ से ही चिपका रहता था। शक्ति की कमी रही होगी, पर ऊर्जा की कमी नहीं थी; क्योंकि मैं अपने ढंग से सदा ही अधिक काम करने वाला प्रसिद्ध रहा हूँ। या शायद, ऊर्जा अधिक नहीं थी, पर जो थी, उसे मैंने बिखरने नहीं दिया।
मुझे अपना जीवन लाहौर से याद आता है। दिल्ली के पुराने शाहदरा जैसे किसी मुहल्ले में ‘भगतां दा चौक’ के पास हरनामसिंह के मकान में हम किरायेदार थे। एक कमरा और रसोई नीचे की मंजिल पर थे और एक कमरा और शौचालय पहली मंजिल पर था। जब किराया बढ़ाने की बात हुई और पिताजी अधिक किराया नहीं दे पाये तो उन्होंने एक कमरा छोड़ दिया। बाद में शायद रसोई भी छोड़ दी थी। ठीक याद नहीं है मुझे। इतना ही याद है कि पहली मंजिल के एक कमरे में हम रहते थे। गर्मियों के दिनों में कमरा तपता था। जैसे-जैसे धूप चढ़ती थी, चारपाई खिसकती जाती थी।
गली में नालियों की उचित व्यवस्था नहीं थी। घर के बाहर गंदा पानी जमा करने के लिए एक गढ़ा था, जिसे हौदी कहते थे। पानी इतना ही बहना चाहिए था, जितना उस हौदी में समा सके। पानी अधिक हो जाता तो गली में बह जाता और वहाँ कीचड़ हो जाता। इसलिए मालिक मकान की ओर से माँ और पिताजी को हिदायत दी गई कि वे पानी अधिक न बहायें। माँ और पिताजी कम-से-कम पानी से नहाते थे। मुझे और मुझसे बड़े भाई भूषण को दूसरे मुहल्ले में अपनी एक भूआ के घर नहाने जाना पड़ता था-जहाँ नालियों का अस्तित्व था।
मेरे सबसे बड़े भाई सोमदेव को हमारी सौतेली दादी ने गोद ले रखा था-उन्हें हम आज भी उसी रिश्ते से चाचाजी पुकारते हैं। वे दादा-दादी के पास स्यालकोट में ही रहते थे। जाने किन कारणों से मेरे दूसरे भाई सुदर्शन और मेरी एकमात्र बहन विमला भी दादी-दादी के पास ही रहते थे। लाहौर में अपनी माँ और पिजाती के साथ मैं, मुझसे बड़ा भाई भूषण और हमारा सबसे छोटा भाई रवीन्द्र थे।
छह वर्ष की अवस्था होने पर मुझे देवसमाज हाई स्कूल लाहौर में भरती करवा दिया गया। उस समय बच्चे-बाजे-गाजे के साथ स्कूल भेजे जाते थे; पर हम उतने समर्थ नहीं थे। पिताजी मुझे अपने साथ ले गये थे। रास्ते में कहीं से सवा रुपये के लड्डू खरीद लिये थे। लड्डू मास्टर रुड़सिंह के हवाले कर मुझे कक्षा में बैठा दिया गया था। उस समय लाहौर में शिक्षा का माध्यम उर्दू ही था। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि बाहर लोग पांजबी बोलते हैं और कक्षा में घुसते ही उर्दू पर क्यों उतर आते हैं।
सन् छियालीस के आसपास ही पिताजी की आँखों की दशा कुछ अधिक बिगड़ गई थी। डॉक्टरी जाँच में वे सरकारी दफ्तर में कार्य करने के सर्वथा अयोग्य पाये गये थे अतः उन्हें प्रायः पच्चीसेक वर्ष की अस्थायी नौकरी से मुक्त कर दिया गया। और कोई चारा न होने के कारण हम लोग स्यालकोट आ गये। अब तक हमारे दादा का देहांत हो चुका था। पुराना मकान पिताजी और चाचाजी की संयुक्त संपत्ति था और नया मकान हमारे दादा, अपनी छोटी पत्नी के नाम कर गये थे। पुराने मकान में नीचे की मंजिल अंधेरी और सीलन भरी थी। वहाँ कोई रहता नहीं था। पहली और दूसरी मंजिल में किरायेदार थे। दूसरी मंजिल पर पिताजी ने अपने लिए कमरा और रसोई किसी प्रकार खाली करा लिये थे। हम लोग वहीं आकर टिके। नीचे की मंजिल का आगे का कमरा कुछ हवादार था। उसी में उन्होंने माँ के गहनों के पूंजी के आधार पर, खेल के सामान की दुकान खोली।
मुझे मुख्य शहर से दूर, जेल की दीवार से लगते हुए गंडासिंह हाई स्कूल में दाखिला दिलाया गया। मेरे बड़े भाई भी इसी स्कूल में थे।
तभी देश का बँटवारा हुआ। एबट रोड पर हमला हुआ तो हमारी सौतेली दादी हमारे बड़े भाई-बहनों के साथ कैंप चली गई। वहाँ से वे लोग भारत आए और चाचाजी के पास जमशेदपुर पहुँच गए। हमारी सगी दादी, दादा के देहांत पर स्यालकोट आयी थीं और तब से हमारे ही साथ थीं। हम लोग भी कैंप में आए। वहाँ से गाड़ी में ‘डेरा बाबा नानक’ के पास रावी के पुल के पाकिस्तानी क्षेत्र में उतार दिए गए। पैदल पुल पर चढ़ने पर हम भारत के क्षेत्र में आ गए, जहाँ से सैनिक ट्रेकों में हमें किसी अस्थायी डेरे पर पहुंचाया गया। डेरा बाबा नानक में एक महीने के लगभग रुके रहकर, अमृतसर और दिल्ली होते हुए हम लोग जमशेदपुर पहुंचे।
चाचाजी टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के ‘टाउन डिपार्टमेंट’ में सैनिटरी इंजीनियर थे। उनके पास तीन कमरों का क्वार्टर था। उनके तब तक आठ बच्चे थे। घर में एक नौकर और एक आया भी थी। अब दस व्यक्ति अटौर आ गए थे। घर छोटा पड़ने लगा। फिर उनके परिवार का वह घर था और हम उनके घर आ पड़े थे। परिस्थितियाँ वैसी ही बन गईं, जैसी कि हो सकती थीं।
पिताजी ने कदमा बाजार में पटरी पर फलों की दुकान लगानी शुरू की। सोमदेव पहले बसों के चेकर हुए, फिर टिस्को में ट्रेसर हो गए। सुदर्शन दिन में पिताजी के साथ दुकान लगाते और रात को नाइट स्कूल में पढ़ते। माँ घर काम करतीं। बहनजी, भूषण, मैं और रवीन्द्र स्कूलों में भेज दिए गए। जिस दिन हम जमशेदपुर में पहुँचे, बहनजी ने मुझे नहलाते हुए बताया कि यहाँ के लोग पंजाबी नहीं बोलते। यहाँ वही भाषा बोलते हैं, जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है। वे स्कूल में हिंदी पढ़ती थीं और मैं उर्दू।
घर (12, स्टाकिंग रोड, जमशेदपुर) के पास उर्दू माध्यम का एक स्कूल था-‘धतकिडीह लोअर प्राइमरी गर्ल्स स्कूल।’ स्कूल लड़कियों का था, पर शायद लड़कियों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए लड़के भी ले लिये जाते थे। मेरे पास ‘स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट’ नहीं था, इसलिए मेरी दूसरी कक्षा की परीक्षा ली गई। मेरे साथ कुछ लड़के भी थे। हम सब के सब उस परीक्षा में फेल हो गये। किंतु मेरे अंक सब से अधिक थे, इसलिए मुझे तीसरी कक्षा में ले लिया गया। कक्षा में आने पर दो अध्यापिकाएँ मुझे बाहर मैदान में ले गई। एकांत में उन्होंने पूछा, ‘‘तुम हिंदू हो ?’’ ‘‘हाँ।’’ मैंने उत्तर दिया। ‘‘तो फिर उर्दू क्यों पढ़ते हो ?’’ ‘‘हम तो उर्दू ही पढ़ते हैं।’’ मेरा उत्तर था। शायद उनके जीवन में पहली बार एक हिन्दू लड़का उर्दू की कक्षा में आया था।
तीसरी कक्षा की परीक्षा में आया था।
तीसरी कक्षा की परीक्षा में मेरा द्वितीय स्थान था। प्रथम स्थान उस लड़के का था जो हमारी क्लास टीचर के पति से ट्यूशन पढ़ता था। पर चौथी से सातवीं कक्षा तक मैं ही प्रथम आया था। वह कभी द्वितीय भी नहीं आया। फिर हम अलग हो गए थे।
चौथी कक्षा में मैं न्यू मिडिल स्कूल में आ गया था। कक्षा में प्रथम आया था। कक्षा का मॉनिटर भी बना। सब से बड़ी उपलब्धि यह थी कि शनिवार के पहले पीरियड में होने वाले वादविवाद में मेरी धाक जम गई थी। छठी कक्षा में ‘एजुकेशन वीक’ के अवसर पर सारे मिडिल स्कूलों की उर्दू वादविवाद प्रतियोगिता में प्रथम रहा था। उसमें मुझे एक मेडल मिला था, जिसे मैं बहुत दिनों तक अपनी कमीज पर टाँगा करता था। विषयवस्तु मुझे पिताजी ने लिख दी थी। उसे मैंने रट लिया था। अनेक बार अनेक लोगों के सामने उस भाषण को मैंने दुहराया था। भाषण-प्रतियोगिताओं का यह सिलसिला बढ़ता ही गया था। आठवीं से ग्यारहवीं तक चारों वर्षों में, एजुकेशन वीक में मैं वाद-विवाद प्रतियोगता में प्रथम रहा। पहले उर्दू में, फिर हिंदी में। बिहार की बच्चों की संस्था ‘किशोर दल’ की प्रतियोगिता में पहले पुरुलिया में और फिर छपरा में उर्दू में प्रथम, लड़कों में प्रथम और सर्वश्रेष्ठ वक्ता के पुरस्कार जीते। कॉलेज में होने वाली अनेक प्रतियोगतिओं के अतिरिक्त बिहार विश्वविद्यालय की ओर से हिंदी और उर्दू की प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कुछ पुरस्कार भी जीते।
छठी कक्षा में ही साहित्यिक रुचि के कुछ मित्र भी संयोग से मिल गए। कक्षा की हस्तलिखित पत्रिका में दो कविताएँ लिखी थीं। वे कविताएँ इसलिए थीं, क्योंकि फुट्टे से नापने पर उसकी पंक्तियाँ बराबर निकलती थीं, और प्रत्येक पंक्ति के अंत में ‘है’ शब्द आता था। सातवीं कक्षा में कुछ कहानियाँ भी लिखीं, जो कक्षा के ही एक मित्र की हस्तलिखित पत्रिका में प्रकाशित हुईं।
इधर चाचाजी ने धनबाद में नयी नौकरी खोज ली थी। उनके परिवार के साथ बड़ी दादी भी चली गई थीं। छोटी दादी अपने सौतेले बेटों से रूठकर जालंधर लौट आयी थीं। हम लोग मकान के लिए कुछ महीने भटक-भटककर कदमा के के.डी. फ्लैटों के आउटहाउस (नौकरों के लिए बने मकान) के दो कमरों में आ गए थे। सोमदेव की शायद कोई पदोन्नति हो गई थी। उन्होंने किसी विश्वविद्यालय से प्राइवेट आई.ए. कर लिया था और शाम को ‘टेक्निकल इंस्टिट्यूट’ में इंजीनियरिंग का कोई डिप्लोमा कर रहे थे। पिताजी और सुदर्शन ने व्यापार कुछ बढ़ा लिया था। एक पक्की दुकान किराए पर ले ली थी। सुदर्शन भैया अंदर की पक्की दुकान पर बैठते थे। पिताजी, भूषण और मैं बाहर पटरी पर दुकान लगाया करते थे।
आठवीं कक्षा में बाहर पटरी पर फल बेचते हुए एक घटना देखकर मैंने एक कहानी ‘हिदोस्ताँ : जनता निशां:’ उर्दू में लिखी थी, जो स्कूल की मुद्रित पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।
उन दिनों के विषय में यही याद है कि कक्षा में मैं प्रथम आता था और भाषण प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतता था इसलिए बाहर पटरी पर फल बेचने और आउटहाउस में रहने बावजूद स्वयं को किसी से हीन नहीं मानता था। फ्लैट में रहने वाले बच्चों से झगड़ा भी होता था, क्योंकि वे अफसरों के बच्चे थे, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते थे और फ्लैटों में रहते थे। पर फ्लैटों में रहने वाला प्रभाकर मेरा मित्र भी था। खेलने के नाम पर हम गुल्ली-डंडे से लेकर क्रिकेट, फुटबाल और वॉलीबाल....सब कुछ खेलते थे, पर मैं कभी अच्छा खिलाड़ी नहीं था। मेरा रिकार्ड है कि मैंने जीवन भर कभी किसी खेल में कोई पुरस्कार नहीं जीता।
सामने वाले मोहन के साथ मिलकर एक छोटा-सा पुस्तकालय खोला था। शायद चार आने महीने पर लोगों को सदस्य बनाते थे और कुछ नयी पुस्तकें लाते थे। उन दिनों उर्दू में ‘खिलौना’, ‘बीसवीं सदी’ और ‘नया अदब’ या ऐसी ही कुछ पत्रिकाएँ पढ़ते थे। प्रेमचन्द का गोदान भी तभी उर्दू में पढ़ा था। ‘जासूसी दुनिया’ बड़ी प्रिय पत्रिका थी। मतीन ने कहीं से यशपाल की वो दुनिया भी लाकर दी थी। मैं, मतीन और नसीम सब ही अफसानानिगार बनने के चक्कर में थे।
हिन्दी में रॉबर्ट ब्लैक, सैक्सटन ब्लैक, जासूस महल, मधूप जासूस इत्यादि तो पढ़ते ही थे। महत्त्वपूर्ण बात यह हुई थी कि बहन जी कॉलेज में पहुंच गई थीं और हिन्दी साहित्य पढ़ रही थीं। तुसली पद्माकर, रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद, निराला पंत और महादेवी की पंक्तियाँ वे अकसर पढ़कर सुनाती थीं और शायद उनके इसी प्रभाव में मेरे मन ने निर्णय किया था कि मैट्रिक के बाद न तो मैं उर्दू पढ़ूँगा, न विज्ञान। मैं तो साहित्य पढ़ूंगा-हिन्दी साहित्य। न बैरिस्टर बनूंगा, न आई.ए.एस. अफसर न इंजीनियर न डॉक्टर। मैं तो बनूंगा लेखक। उन्हीं दिनों मैंने छायावाद कवियों को पढ़कर उन्हीं के शब्दों को लेकर ढेरों प्रेम कविताएं लिख डाली थीं। इन्हीं दिनों लड़कियों के प्रति मन में कुछ आकर्षण भी जागा और मित्रों से यौन संबंधों के विषय में अधकचरा ज्ञान भी प्राप्त हुआ। मैट्रिक (ग्यारहवीं) की परीक्षा देने तक मैं अपना भविष्य तय कर चुका था। यद्यपि पिताजी और तीन बड़े भाइयों की सम्मिलित आय के कारण घर की आर्थिक अवस्था कुछ सुधर चुकी थी और पढ़ने वालों में बहनजी, मैं और रवीन्द्र ही रह गए थे, पर मैं जानता था कि मेरा परिवार मुझे जमशेदपुर से बाहर भेजकर पढ़ाई कराने में आर्थिक रूप से अक्षम है। उसमें मेरी रुचि भी नहीं थी। पर जमशेदपुर औद्योगिक नगर है। यहां के बच्चों और उनके अभिभावकों की महत्त्वाकांक्षा प्रायः इंजीनियर बनने की होती है। मैंने उर्दू माध्यम से विज्ञान के विषयों की परीक्षा दी थी। छिहत्तर प्रतिशत अंक भी आये थे-पर मैं इंजीनियरिंग छोड़, विज्ञान भी पढ़ना नहीं चाहता था। इसीलिए छुट्टियों में वाल्मीकीय रामायण और महाभारत का संक्षिप्त उर्दू संस्करण पढ़ डाला था। पंडित राधेश्याम कथावाचक की रामायण भी उन्हीं दिनों पढ़ी थी। थोड़ी-थोड़ी अंग्रेजी भी पढ़ने लगा था। इसलिए बड़े भैया की अंग्रेजी पुस्तकों में से चुन-चुनकर सरल पुस्तकें पढ़ने का प्रयत्न करता था। जहाँ तक मुझे याद है, मैं उन दिनों पर्ल एस. बक को ही पढ़ पाता था। ‘दि गुड अर्थ’ ‘और ‘ड्रायगान सीड’ उन्हीं दिनों पढ़ी थीं। पढ़ने का यह क्रम आगे की गर्मी की छुट्टियों में भी चलता रहा। मैंने भैया के संग्रह में से पर्ल एस. बक के अतिरिक्त सामरसेट माम को पढ़ा जेन आस्टन और एमिली ब्रांटे की ‘एमा’, ‘प्राइड एंड प्रेजुडिस’ तथा ‘वुदरिंग हाइट्स’ भी तभी पढ़ी थीं।
1957 की जुलाई में मैंने को-आपरेटिव कॉलेज में आई. ए. में प्रवेश लिया और विषय चुने: हिंदी, मनोविज्ञान और तर्कशास्त्र। जो तूफान मचना था, वह मचा। अपरिचितों को लगा, अंक कम होंगे, इसलिए ‘आर्ट्स’ पढ़ रहा है। घरवालों और मेरे अध्यापकों को लगा कि लड़के का दिमाग खराब हो गया है, जो विज्ञान छोड़ कला में आ गया है। पर मेरा वह वय था, जब आदमी आकाश से नीचे देखता ही नहीं। किसी की नहीं सुनी। घरवाले भी मेरे आत्मविश्वास के सामने झुक गए। किसी ने अधिक दबाव नहीं डाला। थोड़ा बहुत कह-कहवाकर चुप हो गए।
उर्दू से हिंदी में आने के लिए एक तिकड़म किया। उन दिनों जमशेदपुर में ‘मुख्य हिंदी’ या मुख्य उर्दू के लिए अंग्रेजी का एक शब्द ‘क्लासिक्स’ प्रयुक्त होता था। मैंने विषय के रूप में क्लासिक्स लिखा। हिंदू लड़के के लिए क्लासिक्स ‘हिंदी’ ही होगी, मानकर मुझे हिंदी की कक्षा में भेज दिया गया।
आरंभ में काफी कठिनाई हुई। हिन्दी के छोटे-छोटे साधारण शब्दों के अर्थ पूछकर मैं अपने अध्यापकों को परेशान किया करता था। जल्दी-जल्दी हिंदी लिख नहीं सकता था, इसलिए कक्षा में उर्दू में नोट्स लिखा करता था। पर दो चार महीनों में अभ्यास हो गया। कक्षा की प्रथम परीक्षा में मैं हिंदी में प्रथम आया था।
को-आपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर में शायद पहला कॉलेज था और अभी बहुत पुराना नहीं था। उसका अपना भवन तक नहीं बना था। इसलिए के. एम. पी. एम. हाई स्कूल के भवन में शाम के समय वह कॉलेज लगता था अध्यापक भी नये थे। पर आज सोचता हूँ तो लगता है कि मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिला, बहुत अच्छे अध्यापक मिले और बहुत अच्छा वातावरण मिला।
कॉलेज में आते ही लेखक मंडल और हिंदी साहित्य परिषद ने मुझे आकृष्ट किया। डॉ. सत्यदेव ओझा लेखक मंडल के अध्यक्ष और संयोजक थे। कॉलेज से उसका कोई संबंध नहीं था, पर कॉलेज के छात्र ही उसमें अपनी रचनाएँ पढ़ते थे और उन पर टिप्पणी करते थे। ‘हिंदी साहित्य परिषद’ कॉलेज की संस्था थी और साहित्यिक गतिविधियों में लगी रहती थी। लेफ्टिनेंट चंद्रभूषण सिन्हा और श्री रमाकांत झा हमारे अन्य अध्यापक थे। यद्यपि लेखक मंडल ओझा जी ही चलाते थे, पर हमारे सर्वप्रिय अध्यापक सिन्हा जी ही थे।
नाटक में अभिनय की लत यहाँ और जुड़ गई। यह अवधि एक नशे की-सी थी। लड़के-लड़कियों के साथ पढ़ना, कहानियाँ और कवितायें लिखना, प्रतियोगताओं में जाना, अभिनय करना, पुरस्कार जीतना....आई. ए. की परीक्षा दी ही थी कि सरिता में नये अंकुर स्तम्भ के अन्तर्गत एक कहानी ‘पानी का जग, गिलास और केतली’ छपी और फरवरी 1960 की कहानी में दो हाथ छपी जिसे अकसर मैंने अपनी पहली प्रकाशित कहानी माना है।
इधर घर में कई परिवर्तन आए थे। घर की आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हो गई थी। हम लोग कदमा के के. डी. फ्लैट का आउटहाउस छोड़कर, साउथ पार्क के एक बड़े भवन के एक अच्छे फ्लैट में आ गए थे। बड़े भैया सोमदेव का विवाह हो गया था। 1959-61 की मेरी कहानियाँ घर के इन्हीं परिवर्तनों पर आधृत हैं। बहन जी का भी विवाह हो गया। मैंने बी. ए. ऑनर्स की परीक्षा दी और आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गया।
रामजस कॉलेज में प्रवेश लिया और होस्टल में डेरा जमाया। दिल्ली बड़ा शहर था, बड़ा विश्वविद्यालय था। मैं परदेसी आदमी, जो छोटे-से राँची विश्वविद्यालय से पढ़कर आया था और जिसके पास स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं था। पर मैं जानता था कि मैं साहित्यकार हूँ, और साहित्यकार का प्रथम लक्षण यही है कि मन की गहराइयों में वह अच्छी तरह जानता है कि वह किसी से हीन नहीं है।
अब सोचा तो लगा कि जमशेदपुर में बहुत अच्छा वातावरण था, जहाँ एक दूसरे को सम्मान दिया जाता था और परस्पर मैत्री-भावना थी। हम बीसेक विद्यार्थी-लड़कियाँ और लड़के-ऐसे भी थे, जो एक दूसरे के घर जाते थे। इकट्ठे घूमते-फिरते थे। परस्पर आकर्षण भी थे। जहाँ अनेक सखा थे, वहीं अनेक सखियाँ भी थीं; पर प्रेम सम्बन्ध कोई भी विकसित नहीं हुआ था।
दिल्ली में उस वातावरण के स्थान पर मात्र उपेक्षा मिली। प्रत्येक व्यक्ति ने हीन सिद्ध करने का प्रयत्न किया-पढ़ाई में, वाद-विवाद प्रतियोगिता में, साहित्य में, धन, पद और सामाजिक सम्मान में। पर यह स्थिति अधिक देर चली नहीं। वाद-विवाद तो मैंने समय नष्ट होने के भय से स्वयं ही छोड़ दिया। रामजस कॉलेज की पत्रिका का छात्र सम्पादक मैं बन गया। होस्टल यूनियन का सेक्रेटरी मैं था। कॉलेज के नाटक का नायक भी मैं ही था। ‘सारिका’ में मोहन राकेश के सम्पादन में ‘होने वाली पत्नी’ कहानी छप गई। और मजे की बात थी कि कॉलेज की परीक्षाओं में प्रथम भी आ गया। स्थिति उतनी खराब नहीं रही।
पर मेरे दादा ने अपनी वैध-अवैध कमाई के आधार पर दो मकान बनवाये थे। एक मकान ‘ट्रंकां वाले बाजार’ के ‘मुहल्ला डिप्टी का बाग’ में था-जो पुराने किस्म का मकान था और किराये पर चढ़ा हुआ था। दूसरा मकान ‘मुहल्ला वाटर वर्क्स में एबट रोड पर था। यह नये क्षेत्र में खुला हवादार मकान था। दूसरा मकान था। इसमें मेरे दादा स्वयं रहते थे। उनकी दो पत्नियाँ थीं। दादा की बड़ी पत्नी-हमारी सगी दादी-अपने पति से अलग, चाचाजी के पास जमशेदपुर में रहतीं थीं। दादा अपनी दूसरी पत्नी से साथ अपने इस मकान में रहते थे। मेरे दादा का नाम हरकिशनदास और दादी का नाम भाइयां देई था। छोटी-दादी मेरी सौतेली दादी-का नाम दुर्गादेवी था। दादा उर्दू और अंग्रेजी जानते थे। शायद मैट्रिक पास थे। दादियाँ दोनों ही निरक्षर थीं।
मेरे पिता-परमानन्द कोहली-की आँखों में बचपन से कुकरे थे। दृष्टि दोषपूर्ण होने के कारण वे सातवीं-आठवीं से आगे नहीं पढ़ सके थे। दादा ने उन्हें स्यालकोट में पुस्तकों और पत्रिकाओं की एक दुकान खोल दी थी। किंतु वे दुकानदार नहीं, साहित्यकार बनना चाहते थे। उन्होंने दो एक कहानियां भी लिखी थीं, जो किसी दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित हुई थी; किंतु न वे साहित्यकार बन सके और न दुकानदार। अंग्रेजों के विरुद्ध किये गये किसी प्रदर्शन में पकड़े गये। दादा जमानत पर न केवल उन्हें छुड़ा लाये, वरन् अपने अंग्रेज अधिकारी से कहकर उन्हें अपने ही विभाग में अस्थायी क्लर्क की नौकरी दिलवा दी। समुचित रूप से शिक्षित न होने और अपने दृष्टिकोण के कारण, उनकी नौकरी न कभी पक्की हो सकी, न उनकी पदोन्नति हुई; दूसरी ओर अपने परिश्रम और अंग्रेज अधिकारी की कृपा के कारण वे नौकरी से निकाले भी नहीं जा सके। जहाँ थे, त्रिशंकु के समान वहीं टंगे रहे।
मेरी माँ-विद्यावंती-स्यालकोट के पास के ही एक गाँव ‘कौलोकी’ के कृषक परिवार से थीं। ‘कौलोकी’ में न स्कूल था, न डाकघर, न अस्पताल, न ही कुछ और। माँ सर्वथा निरक्षर थीं।
मेरा शैशव कभी भी नटखट और खिलंडरे बच्चों का शैशव नहीं रहा। आरम्भ में कदाचित मैं काफी बीमार और रोना बच्चा रहा होऊँगा। शरीर पर फोड़े-फुंसियाँ भी बहुत थीं। अधिकांशतः माँ से ही चिपका रहता था। शक्ति की कमी रही होगी, पर ऊर्जा की कमी नहीं थी; क्योंकि मैं अपने ढंग से सदा ही अधिक काम करने वाला प्रसिद्ध रहा हूँ। या शायद, ऊर्जा अधिक नहीं थी, पर जो थी, उसे मैंने बिखरने नहीं दिया।
मुझे अपना जीवन लाहौर से याद आता है। दिल्ली के पुराने शाहदरा जैसे किसी मुहल्ले में ‘भगतां दा चौक’ के पास हरनामसिंह के मकान में हम किरायेदार थे। एक कमरा और रसोई नीचे की मंजिल पर थे और एक कमरा और शौचालय पहली मंजिल पर था। जब किराया बढ़ाने की बात हुई और पिताजी अधिक किराया नहीं दे पाये तो उन्होंने एक कमरा छोड़ दिया। बाद में शायद रसोई भी छोड़ दी थी। ठीक याद नहीं है मुझे। इतना ही याद है कि पहली मंजिल के एक कमरे में हम रहते थे। गर्मियों के दिनों में कमरा तपता था। जैसे-जैसे धूप चढ़ती थी, चारपाई खिसकती जाती थी।
गली में नालियों की उचित व्यवस्था नहीं थी। घर के बाहर गंदा पानी जमा करने के लिए एक गढ़ा था, जिसे हौदी कहते थे। पानी इतना ही बहना चाहिए था, जितना उस हौदी में समा सके। पानी अधिक हो जाता तो गली में बह जाता और वहाँ कीचड़ हो जाता। इसलिए मालिक मकान की ओर से माँ और पिताजी को हिदायत दी गई कि वे पानी अधिक न बहायें। माँ और पिताजी कम-से-कम पानी से नहाते थे। मुझे और मुझसे बड़े भाई भूषण को दूसरे मुहल्ले में अपनी एक भूआ के घर नहाने जाना पड़ता था-जहाँ नालियों का अस्तित्व था।
मेरे सबसे बड़े भाई सोमदेव को हमारी सौतेली दादी ने गोद ले रखा था-उन्हें हम आज भी उसी रिश्ते से चाचाजी पुकारते हैं। वे दादा-दादी के पास स्यालकोट में ही रहते थे। जाने किन कारणों से मेरे दूसरे भाई सुदर्शन और मेरी एकमात्र बहन विमला भी दादी-दादी के पास ही रहते थे। लाहौर में अपनी माँ और पिजाती के साथ मैं, मुझसे बड़ा भाई भूषण और हमारा सबसे छोटा भाई रवीन्द्र थे।
छह वर्ष की अवस्था होने पर मुझे देवसमाज हाई स्कूल लाहौर में भरती करवा दिया गया। उस समय बच्चे-बाजे-गाजे के साथ स्कूल भेजे जाते थे; पर हम उतने समर्थ नहीं थे। पिताजी मुझे अपने साथ ले गये थे। रास्ते में कहीं से सवा रुपये के लड्डू खरीद लिये थे। लड्डू मास्टर रुड़सिंह के हवाले कर मुझे कक्षा में बैठा दिया गया था। उस समय लाहौर में शिक्षा का माध्यम उर्दू ही था। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि बाहर लोग पांजबी बोलते हैं और कक्षा में घुसते ही उर्दू पर क्यों उतर आते हैं।
सन् छियालीस के आसपास ही पिताजी की आँखों की दशा कुछ अधिक बिगड़ गई थी। डॉक्टरी जाँच में वे सरकारी दफ्तर में कार्य करने के सर्वथा अयोग्य पाये गये थे अतः उन्हें प्रायः पच्चीसेक वर्ष की अस्थायी नौकरी से मुक्त कर दिया गया। और कोई चारा न होने के कारण हम लोग स्यालकोट आ गये। अब तक हमारे दादा का देहांत हो चुका था। पुराना मकान पिताजी और चाचाजी की संयुक्त संपत्ति था और नया मकान हमारे दादा, अपनी छोटी पत्नी के नाम कर गये थे। पुराने मकान में नीचे की मंजिल अंधेरी और सीलन भरी थी। वहाँ कोई रहता नहीं था। पहली और दूसरी मंजिल में किरायेदार थे। दूसरी मंजिल पर पिताजी ने अपने लिए कमरा और रसोई किसी प्रकार खाली करा लिये थे। हम लोग वहीं आकर टिके। नीचे की मंजिल का आगे का कमरा कुछ हवादार था। उसी में उन्होंने माँ के गहनों के पूंजी के आधार पर, खेल के सामान की दुकान खोली।
मुझे मुख्य शहर से दूर, जेल की दीवार से लगते हुए गंडासिंह हाई स्कूल में दाखिला दिलाया गया। मेरे बड़े भाई भी इसी स्कूल में थे।
तभी देश का बँटवारा हुआ। एबट रोड पर हमला हुआ तो हमारी सौतेली दादी हमारे बड़े भाई-बहनों के साथ कैंप चली गई। वहाँ से वे लोग भारत आए और चाचाजी के पास जमशेदपुर पहुँच गए। हमारी सगी दादी, दादा के देहांत पर स्यालकोट आयी थीं और तब से हमारे ही साथ थीं। हम लोग भी कैंप में आए। वहाँ से गाड़ी में ‘डेरा बाबा नानक’ के पास रावी के पुल के पाकिस्तानी क्षेत्र में उतार दिए गए। पैदल पुल पर चढ़ने पर हम भारत के क्षेत्र में आ गए, जहाँ से सैनिक ट्रेकों में हमें किसी अस्थायी डेरे पर पहुंचाया गया। डेरा बाबा नानक में एक महीने के लगभग रुके रहकर, अमृतसर और दिल्ली होते हुए हम लोग जमशेदपुर पहुंचे।
चाचाजी टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के ‘टाउन डिपार्टमेंट’ में सैनिटरी इंजीनियर थे। उनके पास तीन कमरों का क्वार्टर था। उनके तब तक आठ बच्चे थे। घर में एक नौकर और एक आया भी थी। अब दस व्यक्ति अटौर आ गए थे। घर छोटा पड़ने लगा। फिर उनके परिवार का वह घर था और हम उनके घर आ पड़े थे। परिस्थितियाँ वैसी ही बन गईं, जैसी कि हो सकती थीं।
पिताजी ने कदमा बाजार में पटरी पर फलों की दुकान लगानी शुरू की। सोमदेव पहले बसों के चेकर हुए, फिर टिस्को में ट्रेसर हो गए। सुदर्शन दिन में पिताजी के साथ दुकान लगाते और रात को नाइट स्कूल में पढ़ते। माँ घर काम करतीं। बहनजी, भूषण, मैं और रवीन्द्र स्कूलों में भेज दिए गए। जिस दिन हम जमशेदपुर में पहुँचे, बहनजी ने मुझे नहलाते हुए बताया कि यहाँ के लोग पंजाबी नहीं बोलते। यहाँ वही भाषा बोलते हैं, जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है। वे स्कूल में हिंदी पढ़ती थीं और मैं उर्दू।
घर (12, स्टाकिंग रोड, जमशेदपुर) के पास उर्दू माध्यम का एक स्कूल था-‘धतकिडीह लोअर प्राइमरी गर्ल्स स्कूल।’ स्कूल लड़कियों का था, पर शायद लड़कियों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए लड़के भी ले लिये जाते थे। मेरे पास ‘स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट’ नहीं था, इसलिए मेरी दूसरी कक्षा की परीक्षा ली गई। मेरे साथ कुछ लड़के भी थे। हम सब के सब उस परीक्षा में फेल हो गये। किंतु मेरे अंक सब से अधिक थे, इसलिए मुझे तीसरी कक्षा में ले लिया गया। कक्षा में आने पर दो अध्यापिकाएँ मुझे बाहर मैदान में ले गई। एकांत में उन्होंने पूछा, ‘‘तुम हिंदू हो ?’’ ‘‘हाँ।’’ मैंने उत्तर दिया। ‘‘तो फिर उर्दू क्यों पढ़ते हो ?’’ ‘‘हम तो उर्दू ही पढ़ते हैं।’’ मेरा उत्तर था। शायद उनके जीवन में पहली बार एक हिन्दू लड़का उर्दू की कक्षा में आया था।
तीसरी कक्षा की परीक्षा में आया था।
तीसरी कक्षा की परीक्षा में मेरा द्वितीय स्थान था। प्रथम स्थान उस लड़के का था जो हमारी क्लास टीचर के पति से ट्यूशन पढ़ता था। पर चौथी से सातवीं कक्षा तक मैं ही प्रथम आया था। वह कभी द्वितीय भी नहीं आया। फिर हम अलग हो गए थे।
चौथी कक्षा में मैं न्यू मिडिल स्कूल में आ गया था। कक्षा में प्रथम आया था। कक्षा का मॉनिटर भी बना। सब से बड़ी उपलब्धि यह थी कि शनिवार के पहले पीरियड में होने वाले वादविवाद में मेरी धाक जम गई थी। छठी कक्षा में ‘एजुकेशन वीक’ के अवसर पर सारे मिडिल स्कूलों की उर्दू वादविवाद प्रतियोगिता में प्रथम रहा था। उसमें मुझे एक मेडल मिला था, जिसे मैं बहुत दिनों तक अपनी कमीज पर टाँगा करता था। विषयवस्तु मुझे पिताजी ने लिख दी थी। उसे मैंने रट लिया था। अनेक बार अनेक लोगों के सामने उस भाषण को मैंने दुहराया था। भाषण-प्रतियोगिताओं का यह सिलसिला बढ़ता ही गया था। आठवीं से ग्यारहवीं तक चारों वर्षों में, एजुकेशन वीक में मैं वाद-विवाद प्रतियोगता में प्रथम रहा। पहले उर्दू में, फिर हिंदी में। बिहार की बच्चों की संस्था ‘किशोर दल’ की प्रतियोगिता में पहले पुरुलिया में और फिर छपरा में उर्दू में प्रथम, लड़कों में प्रथम और सर्वश्रेष्ठ वक्ता के पुरस्कार जीते। कॉलेज में होने वाली अनेक प्रतियोगतिओं के अतिरिक्त बिहार विश्वविद्यालय की ओर से हिंदी और उर्दू की प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कुछ पुरस्कार भी जीते।
छठी कक्षा में ही साहित्यिक रुचि के कुछ मित्र भी संयोग से मिल गए। कक्षा की हस्तलिखित पत्रिका में दो कविताएँ लिखी थीं। वे कविताएँ इसलिए थीं, क्योंकि फुट्टे से नापने पर उसकी पंक्तियाँ बराबर निकलती थीं, और प्रत्येक पंक्ति के अंत में ‘है’ शब्द आता था। सातवीं कक्षा में कुछ कहानियाँ भी लिखीं, जो कक्षा के ही एक मित्र की हस्तलिखित पत्रिका में प्रकाशित हुईं।
इधर चाचाजी ने धनबाद में नयी नौकरी खोज ली थी। उनके परिवार के साथ बड़ी दादी भी चली गई थीं। छोटी दादी अपने सौतेले बेटों से रूठकर जालंधर लौट आयी थीं। हम लोग मकान के लिए कुछ महीने भटक-भटककर कदमा के के.डी. फ्लैटों के आउटहाउस (नौकरों के लिए बने मकान) के दो कमरों में आ गए थे। सोमदेव की शायद कोई पदोन्नति हो गई थी। उन्होंने किसी विश्वविद्यालय से प्राइवेट आई.ए. कर लिया था और शाम को ‘टेक्निकल इंस्टिट्यूट’ में इंजीनियरिंग का कोई डिप्लोमा कर रहे थे। पिताजी और सुदर्शन ने व्यापार कुछ बढ़ा लिया था। एक पक्की दुकान किराए पर ले ली थी। सुदर्शन भैया अंदर की पक्की दुकान पर बैठते थे। पिताजी, भूषण और मैं बाहर पटरी पर दुकान लगाया करते थे।
आठवीं कक्षा में बाहर पटरी पर फल बेचते हुए एक घटना देखकर मैंने एक कहानी ‘हिदोस्ताँ : जनता निशां:’ उर्दू में लिखी थी, जो स्कूल की मुद्रित पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।
उन दिनों के विषय में यही याद है कि कक्षा में मैं प्रथम आता था और भाषण प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतता था इसलिए बाहर पटरी पर फल बेचने और आउटहाउस में रहने बावजूद स्वयं को किसी से हीन नहीं मानता था। फ्लैट में रहने वाले बच्चों से झगड़ा भी होता था, क्योंकि वे अफसरों के बच्चे थे, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते थे और फ्लैटों में रहते थे। पर फ्लैटों में रहने वाला प्रभाकर मेरा मित्र भी था। खेलने के नाम पर हम गुल्ली-डंडे से लेकर क्रिकेट, फुटबाल और वॉलीबाल....सब कुछ खेलते थे, पर मैं कभी अच्छा खिलाड़ी नहीं था। मेरा रिकार्ड है कि मैंने जीवन भर कभी किसी खेल में कोई पुरस्कार नहीं जीता।
सामने वाले मोहन के साथ मिलकर एक छोटा-सा पुस्तकालय खोला था। शायद चार आने महीने पर लोगों को सदस्य बनाते थे और कुछ नयी पुस्तकें लाते थे। उन दिनों उर्दू में ‘खिलौना’, ‘बीसवीं सदी’ और ‘नया अदब’ या ऐसी ही कुछ पत्रिकाएँ पढ़ते थे। प्रेमचन्द का गोदान भी तभी उर्दू में पढ़ा था। ‘जासूसी दुनिया’ बड़ी प्रिय पत्रिका थी। मतीन ने कहीं से यशपाल की वो दुनिया भी लाकर दी थी। मैं, मतीन और नसीम सब ही अफसानानिगार बनने के चक्कर में थे।
हिन्दी में रॉबर्ट ब्लैक, सैक्सटन ब्लैक, जासूस महल, मधूप जासूस इत्यादि तो पढ़ते ही थे। महत्त्वपूर्ण बात यह हुई थी कि बहन जी कॉलेज में पहुंच गई थीं और हिन्दी साहित्य पढ़ रही थीं। तुसली पद्माकर, रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद, निराला पंत और महादेवी की पंक्तियाँ वे अकसर पढ़कर सुनाती थीं और शायद उनके इसी प्रभाव में मेरे मन ने निर्णय किया था कि मैट्रिक के बाद न तो मैं उर्दू पढ़ूँगा, न विज्ञान। मैं तो साहित्य पढ़ूंगा-हिन्दी साहित्य। न बैरिस्टर बनूंगा, न आई.ए.एस. अफसर न इंजीनियर न डॉक्टर। मैं तो बनूंगा लेखक। उन्हीं दिनों मैंने छायावाद कवियों को पढ़कर उन्हीं के शब्दों को लेकर ढेरों प्रेम कविताएं लिख डाली थीं। इन्हीं दिनों लड़कियों के प्रति मन में कुछ आकर्षण भी जागा और मित्रों से यौन संबंधों के विषय में अधकचरा ज्ञान भी प्राप्त हुआ। मैट्रिक (ग्यारहवीं) की परीक्षा देने तक मैं अपना भविष्य तय कर चुका था। यद्यपि पिताजी और तीन बड़े भाइयों की सम्मिलित आय के कारण घर की आर्थिक अवस्था कुछ सुधर चुकी थी और पढ़ने वालों में बहनजी, मैं और रवीन्द्र ही रह गए थे, पर मैं जानता था कि मेरा परिवार मुझे जमशेदपुर से बाहर भेजकर पढ़ाई कराने में आर्थिक रूप से अक्षम है। उसमें मेरी रुचि भी नहीं थी। पर जमशेदपुर औद्योगिक नगर है। यहां के बच्चों और उनके अभिभावकों की महत्त्वाकांक्षा प्रायः इंजीनियर बनने की होती है। मैंने उर्दू माध्यम से विज्ञान के विषयों की परीक्षा दी थी। छिहत्तर प्रतिशत अंक भी आये थे-पर मैं इंजीनियरिंग छोड़, विज्ञान भी पढ़ना नहीं चाहता था। इसीलिए छुट्टियों में वाल्मीकीय रामायण और महाभारत का संक्षिप्त उर्दू संस्करण पढ़ डाला था। पंडित राधेश्याम कथावाचक की रामायण भी उन्हीं दिनों पढ़ी थी। थोड़ी-थोड़ी अंग्रेजी भी पढ़ने लगा था। इसलिए बड़े भैया की अंग्रेजी पुस्तकों में से चुन-चुनकर सरल पुस्तकें पढ़ने का प्रयत्न करता था। जहाँ तक मुझे याद है, मैं उन दिनों पर्ल एस. बक को ही पढ़ पाता था। ‘दि गुड अर्थ’ ‘और ‘ड्रायगान सीड’ उन्हीं दिनों पढ़ी थीं। पढ़ने का यह क्रम आगे की गर्मी की छुट्टियों में भी चलता रहा। मैंने भैया के संग्रह में से पर्ल एस. बक के अतिरिक्त सामरसेट माम को पढ़ा जेन आस्टन और एमिली ब्रांटे की ‘एमा’, ‘प्राइड एंड प्रेजुडिस’ तथा ‘वुदरिंग हाइट्स’ भी तभी पढ़ी थीं।
1957 की जुलाई में मैंने को-आपरेटिव कॉलेज में आई. ए. में प्रवेश लिया और विषय चुने: हिंदी, मनोविज्ञान और तर्कशास्त्र। जो तूफान मचना था, वह मचा। अपरिचितों को लगा, अंक कम होंगे, इसलिए ‘आर्ट्स’ पढ़ रहा है। घरवालों और मेरे अध्यापकों को लगा कि लड़के का दिमाग खराब हो गया है, जो विज्ञान छोड़ कला में आ गया है। पर मेरा वह वय था, जब आदमी आकाश से नीचे देखता ही नहीं। किसी की नहीं सुनी। घरवाले भी मेरे आत्मविश्वास के सामने झुक गए। किसी ने अधिक दबाव नहीं डाला। थोड़ा बहुत कह-कहवाकर चुप हो गए।
उर्दू से हिंदी में आने के लिए एक तिकड़म किया। उन दिनों जमशेदपुर में ‘मुख्य हिंदी’ या मुख्य उर्दू के लिए अंग्रेजी का एक शब्द ‘क्लासिक्स’ प्रयुक्त होता था। मैंने विषय के रूप में क्लासिक्स लिखा। हिंदू लड़के के लिए क्लासिक्स ‘हिंदी’ ही होगी, मानकर मुझे हिंदी की कक्षा में भेज दिया गया।
आरंभ में काफी कठिनाई हुई। हिन्दी के छोटे-छोटे साधारण शब्दों के अर्थ पूछकर मैं अपने अध्यापकों को परेशान किया करता था। जल्दी-जल्दी हिंदी लिख नहीं सकता था, इसलिए कक्षा में उर्दू में नोट्स लिखा करता था। पर दो चार महीनों में अभ्यास हो गया। कक्षा की प्रथम परीक्षा में मैं हिंदी में प्रथम आया था।
को-आपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर में शायद पहला कॉलेज था और अभी बहुत पुराना नहीं था। उसका अपना भवन तक नहीं बना था। इसलिए के. एम. पी. एम. हाई स्कूल के भवन में शाम के समय वह कॉलेज लगता था अध्यापक भी नये थे। पर आज सोचता हूँ तो लगता है कि मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिला, बहुत अच्छे अध्यापक मिले और बहुत अच्छा वातावरण मिला।
कॉलेज में आते ही लेखक मंडल और हिंदी साहित्य परिषद ने मुझे आकृष्ट किया। डॉ. सत्यदेव ओझा लेखक मंडल के अध्यक्ष और संयोजक थे। कॉलेज से उसका कोई संबंध नहीं था, पर कॉलेज के छात्र ही उसमें अपनी रचनाएँ पढ़ते थे और उन पर टिप्पणी करते थे। ‘हिंदी साहित्य परिषद’ कॉलेज की संस्था थी और साहित्यिक गतिविधियों में लगी रहती थी। लेफ्टिनेंट चंद्रभूषण सिन्हा और श्री रमाकांत झा हमारे अन्य अध्यापक थे। यद्यपि लेखक मंडल ओझा जी ही चलाते थे, पर हमारे सर्वप्रिय अध्यापक सिन्हा जी ही थे।
नाटक में अभिनय की लत यहाँ और जुड़ गई। यह अवधि एक नशे की-सी थी। लड़के-लड़कियों के साथ पढ़ना, कहानियाँ और कवितायें लिखना, प्रतियोगताओं में जाना, अभिनय करना, पुरस्कार जीतना....आई. ए. की परीक्षा दी ही थी कि सरिता में नये अंकुर स्तम्भ के अन्तर्गत एक कहानी ‘पानी का जग, गिलास और केतली’ छपी और फरवरी 1960 की कहानी में दो हाथ छपी जिसे अकसर मैंने अपनी पहली प्रकाशित कहानी माना है।
इधर घर में कई परिवर्तन आए थे। घर की आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हो गई थी। हम लोग कदमा के के. डी. फ्लैट का आउटहाउस छोड़कर, साउथ पार्क के एक बड़े भवन के एक अच्छे फ्लैट में आ गए थे। बड़े भैया सोमदेव का विवाह हो गया था। 1959-61 की मेरी कहानियाँ घर के इन्हीं परिवर्तनों पर आधृत हैं। बहन जी का भी विवाह हो गया। मैंने बी. ए. ऑनर्स की परीक्षा दी और आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गया।
रामजस कॉलेज में प्रवेश लिया और होस्टल में डेरा जमाया। दिल्ली बड़ा शहर था, बड़ा विश्वविद्यालय था। मैं परदेसी आदमी, जो छोटे-से राँची विश्वविद्यालय से पढ़कर आया था और जिसके पास स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं था। पर मैं जानता था कि मैं साहित्यकार हूँ, और साहित्यकार का प्रथम लक्षण यही है कि मन की गहराइयों में वह अच्छी तरह जानता है कि वह किसी से हीन नहीं है।
अब सोचा तो लगा कि जमशेदपुर में बहुत अच्छा वातावरण था, जहाँ एक दूसरे को सम्मान दिया जाता था और परस्पर मैत्री-भावना थी। हम बीसेक विद्यार्थी-लड़कियाँ और लड़के-ऐसे भी थे, जो एक दूसरे के घर जाते थे। इकट्ठे घूमते-फिरते थे। परस्पर आकर्षण भी थे। जहाँ अनेक सखा थे, वहीं अनेक सखियाँ भी थीं; पर प्रेम सम्बन्ध कोई भी विकसित नहीं हुआ था।
दिल्ली में उस वातावरण के स्थान पर मात्र उपेक्षा मिली। प्रत्येक व्यक्ति ने हीन सिद्ध करने का प्रयत्न किया-पढ़ाई में, वाद-विवाद प्रतियोगिता में, साहित्य में, धन, पद और सामाजिक सम्मान में। पर यह स्थिति अधिक देर चली नहीं। वाद-विवाद तो मैंने समय नष्ट होने के भय से स्वयं ही छोड़ दिया। रामजस कॉलेज की पत्रिका का छात्र सम्पादक मैं बन गया। होस्टल यूनियन का सेक्रेटरी मैं था। कॉलेज के नाटक का नायक भी मैं ही था। ‘सारिका’ में मोहन राकेश के सम्पादन में ‘होने वाली पत्नी’ कहानी छप गई। और मजे की बात थी कि कॉलेज की परीक्षाओं में प्रथम भी आ गया। स्थिति उतनी खराब नहीं रही।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book